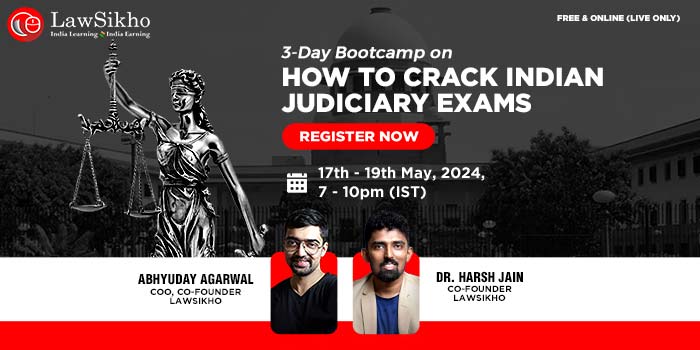यह लेख Chandan Kumar ने लिखा है। इस लेख में भारत की न्यायपालिका की सक्रियता (एक्टिविज्म) और अतिरेक (ओवररीच) के ऊपर चर्चा करते हुए, उदाहरणों के साथ इन्हें समझाया है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारत एक लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) राष्ट्र है जिसमें राजनीतिक शक्ति की तीन शाखाएँ हैं: विधायिका (लेजिस्लेटिव), कार्यकारी (एग्जीक्यूटिव) शाखा और न्यायपालिका (जुडिशयरी) शाखा। जनता और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रत्येक शाखा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। विधायी शक्ति राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंट) करती है और प्रस्तावित (प्रोपोज़) करती है, और इसके एजेंट के रूप में, कानूनों के संदर्भ में समाज के सामान्य नियमों को लागू भी करती है। कार्यपालिका के पास ऐसे कानूनों और आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका पालन सभी लोग करते हैं और कोई उल्लंघन नहीं होता है। तीसरी शाखा, न्यायपालिका, कानून की समीक्षा (रिव्यु) करती है, कानून की व्याख्या (इन्टरप्रेट) करती है, और कानूनों को कायम रखते हुए विवादों का न्याय करती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। भारतीय संविधान ने इन विभाजनों को एक ऐसी संरचना (स्ट्रक्चर) में विभाजित किया है जो उन्हें शक्तियों के पृथक्करण (सेपेरशन ऑफ़ पावर्स) की अवधारणा (कांसेप्ट) के आधार पर अन्य शाखाओं के कर्तव्यों में घुसपैठ (इंट्रूड) या अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) किए बिना व्यक्तियों के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। वे नियंत्रण और संतुलन का एक तंत्र रखने के लिए काम करते हैं ताकि किसी एक शाखा का अन्य की तुलना में अधिक नियंत्रण न हो जाए।
न्यायपालिका, जिसे सरकार की न्यायिक शाखा के रूप में भी जाना जाता है, शायद तीनों शाखाओं में सबसे प्रमुख है। यह सरकारी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक (कम्पोनेट) है और हमारे देश के सुचारू (स्मूथ) कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायपालिका सभी शाखाओं के बीच शक्तियों का संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य रखती है और सरकारों द्वारा कानूनों की व्याख्या करने के लिए देखा जाता है, और लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी ओर रुख करते हैं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि, “एक राष्ट्र के लोग कार्यपालिका (राजा), या विधायिका में विश्वास खो सकते हैं, लेकिन यह एक बुरा दिन होगा यदि वे अपनी न्यायपालिका में अपना विश्वास खो देते हैं। न्यायपालिका मानवाधिकारों (ह्यूमन राइट्स) और नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिबर्टीज) की संरक्षक है।”
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विकसित संस्कृति और समुदाय से निपटने के लिए, न्यायपालिका की पारंपरिक स्थिति को अधिक सक्रिय भागीदारी (एक्टिव पार्टिसिपेटरी) की भूमिका में बदला जा रहा है। भारतीय न्यायपालिका को कभी-कभी लोकतंत्र के “प्रहरी” के रूप में जाना जाता है, और न्याय के समान और निष्पक्ष होने के लिए और न्यायपालिका के लिए अन्य दो शाखाओं पर, संवैधानिक उल्लंघन के मामलों में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होने के लिए इसे स्वायत्त (ऑटोनोमॉस) और सभी कार्यकारी हस्तक्षेप से ऊपर होना चाहिए। संविधान, जो देश का सर्वोच्च कानून है, में अस्पष्ट शब्दावली (वेग टर्मिनोलॉजी) भी है। यह कानून के शासन को भी परिभाषित करता है, जो देश के कानूनी ढांचे की नींव है। अलग-अलग मौकों पर लोगों के अलग-अलग समूह इस शब्द की अलग-अलग व्याख्या करते हैं। नतीजतन, अधिकारियों के लिए अपने अधिकार के बारे में संघर्ष करना आम बात है। नतीजतन, एक स्वायत्त न्यायपालिका प्राधिकरण, संतुलन के रखरखाव में सहायता करेगी।
न्यायिक समीक्षा (जुडिशियल रिव्यु)
न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सर्वोच्च कानून की अखंडता और शक्तियों के अत्याचार से स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए लागू होता है। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका को विधायी निकायों द्वारा किए गए वैधानिक अधिनियमों की जांच करने की शक्ति है। भारत का संविधान, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का पहली बार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मार्बरी बनाम मैडिसन के मामले में इस्तेमाल और विकसित किया गया था। इसने स्थापित किया कि न्यायपालिका के पास यह घोषित करने की पूर्ण शक्ति और जिम्मेदारी है कि कानून क्या है, और यह भी कि संघीय न्यायालय के पास विधायी अधिनियम को बल देने से इनकार करने का अधिकार है, जो कि न्यायालय की संविधान की अवधारणा के विपरीत प्रतीत होता है।
इसी तरह, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लगातार मान्यता दी है, यह तर्क देते हुए कि यह शक्ति एक लिखित संविधान में निहित है, जब तक कि संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध (प्रोहिबिट) न हो। इसने फैसला सुनाया है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति कानून के प्रावधानों के तहत मान्य है जो इसकी श्रेष्ठता का दावा करती है। ऐसी न्यायिक समीक्षा शक्तियाँ, न्यायिक को संवैधानिक संरचना की अन्य शाखाओं से ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए दी जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226, 141, 142 और 144 विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं, जो कि व्यापक क्षेत्राधिकारों, अधिकारियों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ संवैधानिक उद्देश्यों के आलोक में है।
भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। इन उदाहरणों में शंकरी प्रसाद, इंदिरा गांधी, केशवानंद भारती, सज्जन सिंह, मिनर्वा मिल्स और कई अन्य मामले शामिल हैं। माननीय न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में कहा कि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान का एक अंतर्निहित तत्व (इन्हेरेंट एलिमेंट) बन गया है, और उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को वैधानिक प्रावधानों की विधायी क्षमता निर्धारित करने की शक्ति सौंपी गई थी।
फिर एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के त्रि-आयामी दायरे की घोषणा की: शुरू में, कार्यकारी कार्रवाई में न्याय सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, और तीसरा, संघ और राज्यों के बीच विधायी क्षमता के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए।
लोगों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के महत्व को समझने के लिए, न्यायमूर्ति ए एस आनंद ने “न्यायिक समीक्षा – न्यायिक सक्रियता – सावधानी की आवश्यकता” को संबोधित करते हुए अपना विचार व्यक्त किया कि, “विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ,राज्य के तीन समन्वय अंग (कोआर्डिनेट ऑर्गन्स) हैं। ये तीनों संविधान से बंधे हैं। कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों, विधायिका का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्यों के रूप में निर्वाचित उम्मीदवारों और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संविधान की तीसरी अनुसूची द्वारा निर्धारित शपथ लेनी होती है। ये सभी संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं।
इसलिए, जब यह कहा जाता है कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि विधायिका और कार्यपालिका समान रूप से संविधान की रक्षा करने के लिए नहीं हैं। हालांकि, राष्ट्र की प्रगति के लिए यह जरूरी है कि राज्य के तीनों अंग पूर्ण सद्भाव (हारमनी) में काम करें। एक न्यायिक निर्णय विधायिका या कार्यपालिका के निर्णय को ‘कलंकित या वैधीकृत’ करता है। किसी भी मामले में अदालत न तो किसी विधायी नीति को मंजूरी देती है और न ही उसकी निंदा करती है, न ही उसकी समझदारी या समीचीनता (एक्सपीडिएन्सी) से कोई सरोकार (कंसर्न) है। इसका सरोकार केवल यह निर्धारित करना है कि क्या कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या इसके विपरीत है। इसमें अक्सर क़ानून की तर्कसंगतता पर विचार करना शामिल होता है। इसी तरह, जहां अदालत किसी कार्यकारी आदेश को रद्द करती है, वह टकराव की भावना से या अपनी श्रेष्ठता का दावा करने के लिए नहीं बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों और कानून की महिमा के निर्वहन में ऐसा करती है। उन सभी मामलों में, अदालत न्यायिक प्रहरी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है।”
हम उपरोक्त अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अदालत का काम यह देखना है कि कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, देश में चाहे कुछ भी हो, निष्पक्ष या अनुचित, न्यायिक प्रणाली को अपने दायित्वों को अपने भीतर पूरा करना चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी अन्य शाखा का कोई कार्य उसके निर्णयों से बाधित नहीं होता है।
न्यायिक सक्रियता की धारणा और इसके अतिरेक (नोशन ऑफ़ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इट्स ओवररीच)
विधायिका और कार्यपालिका, औसत भारतीय निवासी की राय में, लोगों के प्रति अपनी प्रिय जिम्मेदारियों में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कार्यकारी और विधायी शाखाओं को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। नागरिकों से उनकी निकटता के कारण, उन्हें उच्च मानकों पर रखा जाता है और यदि उनका आचरण प्रत्याशित रूपरेखा को पूरा नहीं करता है, तो उन्हें अक्सर दंडित किया जाता है। औसत व्यक्ति का मानना है कि सरकार इतनी निराश और परित्यक्त हो गई है कि उनके पास अपनी चिंताओं को अदालतों तक ले जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इन चिंताओं के जवाब में न्यायिक प्रणाली ने एक सक्रिय रुख अपनाया है। भारत में, न्यायिक सक्रियता बढ़ी है और भारतीय लोगों के बीच जबरदस्त विश्वसनीयता भी हासिल की गयी है।
न्यायिक सक्रियता (जुडिशियल एक्टिविज्म)
न्यायिक सक्रियता ,न्यायिक समीक्षा और न्यायिक विचारधारा का विस्तार है जो न्यायाधीशों को पारंपरिक और स्थापित मिसालों से हटने और नई प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह न्यायपालिका को अन्याय के निवारण के लिए अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि अन्य सरकारी एजेंसियां उनकी ओर से काम कर रही हैं। एक विकसित दुनिया में, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) का एक जटिल चरण है। न्यायिक सक्रियता वह तंत्र है जिसके द्वारा न्यायपालिका विधायिका की भूमिका ग्रहण करती है और नए कानूनों और विनियमों का प्रस्ताव करती है, जिन्हें विधायी निकाय को इसके बजाय अधिनियमित करना चाहिए था। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार, न्यायिक सक्रियतावाद का अर्थ है “न्यायिक निर्णय लेने का एक दर्शन जिसके द्वारा न्यायाधीश सार्वजनिक नीति के बारे में अपने व्यक्तिगत विचारों को अन्य कारकों के साथ, अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने की अनुमति देते हैं। इस सुझाव के साथ कि इस दर्शन के अनुयायी संवैधानिक उल्लंघन पाते हैं और मिसाल की अनदेखी करने को तैयार हैं।”
न्यायिक सक्रियता को क्रियान्वित (एक्सेक्यूट) करने के कई तरीके हैं, जिनमें जनहित याचिका (पी आई एल) सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इस तथ्य के बावजूद कि जनहित याचिका का सिद्धांत वास्तव में न्यायिक सक्रियता का ही उत्पाद है, यह न्यायपालिका के लिए न्यायिक सक्रियता को संबोधित करने के लिए एक प्रभावी तरीका के रूप में उभरा है। भारत में, जनहित याचिका के माध्यम से वंचित लोगों को राहत देने और न्याय दिलाने के माध्यम से न्यायिक सक्रियता ने अधिक दयालु चेहरे पर कब्जा कर लिया है। जब कोई मामला अदालत में लाया जाता है, तो अदालत आमतौर पर इसकी जांच करेगी और निर्णय देगी। हालांकि, देश की विशाल जरूरतों के आलोक में, न्यायपालिका ने महसूस किया कि जनता के प्रति उसकी भी जिम्मेदारी है, न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए उसे एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और राष्ट्र में कोई भी प्राधिकरण इसे नहीं ले सकता है, और कोई भी कार्रवाई जो उस विश्वास को खतरे में डालती है और विवाद को जन्म देती है।
जब इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान 1975 और 1977 के बीच कई घटनाएं हुईं, जिसमें मौलिक मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ, और उस समय अदालत चुप रही, उसके बाद न्यायिक सक्रियता बढ़ी और कई सक्रिय न्यायाधीश जैसे पी.एन. भगवती, वी.आर. कृष्णा अय्यर और अन्य ने इन उदाहरणों पर ध्यान दिया और इस विषय पर काम किया और इसके विकास में योगदान भी दिया। न्यायिक सक्रियता के कई अन्य उल्लेखनीय तरीकों का उपयोग किया जाता है जिसमें मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के दायरे का विस्तार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या और रचनात्मक तरीके से मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विधियों तक पहुंच और प्रयोग करना शामिल है।
न्यायिक अतिरेक (जुडिशियल ओवररीच)
हालाँकि, जब न्यायपालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो, तो इसका मतलब है की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन शुरू हो गया है, और यहाँ “न्यायिक अतिरेक” शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर न्यायिक साहसिकता (जुडिशियल अडवेंचररिस्म) के रूप में भी जाना जाता है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच की रेखा बहुत छोटी है और इन् दो अवधारणाओं के बीच अंतर करना मुश्किल है। पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि “असंख्य मामलों में अदालतों ने एक हितकारी और सुधारात्मक भूमिका निभाई है। इसके लिए हमारे लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। साथ ही, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिरेक के बीच की विभाजन रेखा बहुत पतली है।” न्यायपालिका कानून की व्याख्या की खोज में नए कानून नहीं बना सकती है या मौजूदा लोगों को बदल नहीं सकती है। इसका कार्य अन्य शाखाओं के कार्यों में हस्तक्षेप करने से बचते हुए कानूनों की व्याख्या करना है। वास्तविक खतरा यह है कि बार-बार हस्तक्षेप से राज्य की दो शाखाओं के शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए।
माननीय न्यायमूर्ति माथुर और काटजू ने एक मामले का फैसला करते हुए कहा था कि, “न्यायिक सक्रियता के नाम पर, न्यायाधीश अपनी सीमाओं को पार नहीं कर सकते हैं और राज्य के किसी अन्य अंग से संबंधित कार्यों को संभालने का प्रयास नहीं कर सकते हैं।” इसमें आगे कहा गया है कि “न्यायाधीशों को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनमें विनम्रता होनी चाहिए और उन्हें सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।” सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी नीति बनाना या उसे लागू करना कार्यपालिका का काम है, और न कि न्यायपालिका का, यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का काम है कि उसका ठीक से पालन हो। लेकिन जब न्यायपालिका मर्यादाओं को भूलकर लोगों का भला करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाती है जो अवांछनीय (अण्डीसायरेबल) है, और कार्यपालिका के काम में बाधा डालती है, तो यह हद से ज्यादा बढ़ जाती है।
‘न्यायिक सक्रियता’ और ‘न्यायिक अतिरेक’ शब्दों में अंतर करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एक वैध न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता आवश्यक है। लेकिन न्यायपालिका, सक्रियता के माध्यम से, केवल मान्यता प्राप्त संस्थान को उसकी अक्षमता या खराबी की स्थिति में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती है; अगर यह किसी अन्य शाखा से संबंधित भूमिका निभाने की कोशिश करता है, तो यह अस्वीकार्य है और इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
वर्तमान न्यायिक सक्रियता का प्रस्ताव, अतिरेक, और इसके प्रभाव
माननीय न्यायालय ने विभिन्न उदाहरणों में अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग किया है और समाज के लिए बेहतर स्थिति बनाने के लिए न्यायिक सक्रियता का कार्य किया है। कानूनी सिद्धांतों और मौजूदा कानूनों को लागू करके, न्यायपालिका ने हाल के दिनों में गलत तरीके से हिरासत, पर्यावरण संबंधी चिंताओं, बच्चों और महिलाओं के अधिकारों, अल्पसंख्यक मामलों, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करते हुए कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जो उभरने और विकास में सहायता करते हैं।
न्यायिक सक्रियता के उदाहरण
न्यायपालिका ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा, नीरजा चौधरी और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे मामलों में एक सक्रिय भूमिका निभाई, समाज के कमजोर वर्गों को जबरन या बंधुआ मजदूरी के खतरे से बचाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या भी की। इन मामलों में, अदालत ने भारत की लोकतांत्रिक समृद्धि को बढ़ावा देने में बच्चों के शैक्षिक, स्वास्थ्य और विकास अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दिया और सरकारों को इस संबंध में नीतियां बनाने के उपायों का पालन करने का निर्देश भी दिया।
अदालत ने एम सी मेहता, शीला बरसे, गौरव जैन, लक्ष्मीकांत पांडेय के मामलों में बाल कल्याण और विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसले सुनाए, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में व्यक्त मानदंडों को भी स्वीकार किया गया था। ये मामले इस विश्लेषण के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वे एक उत्कृष्ट प्रदर्शन (आउटस्टैंडिंग डेमोंस्ट्रेशन) प्रदान करते हैं कि कैसे समाज में कमजोर समूहों के लिए कानूनी व्यवस्था को और अधिक खुला बनाने के लिए भारत में जनहित याचिका में प्रक्रियात्मक प्रगति अदालत के नियमों के सामने नरम हो गई है।
न्यायिक सक्रियता के लिए एक और उल्लेखनीय विषय महिला कल्याण है, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान के मामले में अदालत ने विधायिका की भूमिका निभाई और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए। इसे न्यायिक कानून भी कहा जा सकता है जहां अदालत ने कहा कि इन दिशानिर्देशों का पालन सभी कार्यस्थलों पर अनुच्छेद 141 के तहत कानून के रूप में किया जाना चाहिए, जब तक कि विधायिका इस संबंध में एक विशिष्ट कानून नहीं बनाती है। हालांकि इस संबंध में एक कानून की आवश्यकता पर अदालत ने ध्यान दिया, लेकिन संबंधित विषय के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (सेक्सुअल हरस्मेंट ऑफ़ वीमेन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल) एक्ट) 2013 को तैयार करने में विधायिका को लगभग 16 साल लग गए। न्यायपालिका के इस कार्य की अत्यधिक आलोचना (क्रिटिसाइज़) की गई है क्योंकि यह विधायी क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, लेकिन हम कानून के अधिनियमित होने के लंबे इंतजार से यह अनुमान लगा सकते हैं कि दिशानिर्देश जारी होने के बाद भी, भारत में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता महत्वपूर्ण है ताकि इस समाज में चल रहे मुद्दों का समाधान हो सके।
इसके अलावा, जब अदालत ने कैदियों के अधिकार के जीवंत मुद्दे पर ध्यान दिया क्योंकि उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जा रहा था और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, तो उन्होंने चिंता का फैसला करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, और तब यह देखा जा सकता है कि अदालत ने कैदियों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक फैसले दिए, और साथ ही जोगिंदर कुमार, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, डीके बसु, सुनील बत्रा, हुसैनैरा खातून और इंदर सिंह के मामलों में अवैध हिरासत, पुलिस यातना, फर्जी मुठभेड़, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार पर भी ऐतिहासिक फैसले दिए।
न्यायिक सक्रियता के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ का मामला है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस मामले में अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के अन्य लोगों के लिए हानिकारक और बुरे प्रभावों और इस संबंध में किसी भी वैधानिक प्रावधान की अनुपस्थिति को मान्यता दी थी। इसके बाद, विधायिका ने 2003 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट) नामक एक नया क़ानून बनाया, जिसमें कई सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
न्यायिक अतिरेक के उदाहरण
न्याय प्रदान करने और समाज की बेहतरी के लिए कदम उठाने में न्यायपालिका की सभी सक्रिय भागीदारी के साथ, देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां न्यायपालिका ने अपनी सीमा को पार कर विधायी और कार्यकारी कार्यों में प्रवेश किया है। कुछ उदाहरण जॉली एलएलबी 2 के मामले में सक्रिय सेंसरशिप, एनजेएसी विधेयक को रद्द करना, राष्ट्रगान मामले में देशभक्ति को थोपना और कई अन्य हैं।
जॉली एलएलबी 2 के मामले में सक्रिय सेंसरशिप पहला मामला था जहां अदालत ने सेंसर के रूप में काम किया, जो कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का उल्लंघन था। यहां, अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5B का उल्लंघन करती है, जिसमें बॉम्बे के उच्च न्यायलय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने विभिन्न दृश्यों को ‘आपत्तिजनक’ और मानहानि और अदालत की अवमानना के रूप में सूचीबद्ध करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद, अदालत ने निर्देशक को चार दृश्यों को काटने का आदेश दिया और फिर सीबीएफसी को फिल्म को फिर से प्रमाणित करने का निर्देश भी दिया था।
भारत में, एक कानून है कि अदालतें, अदालतों के अधिकार अधिनियम (कोर्ट्स एक्ट), 1971 को बदनाम करने या कम करने के लिए लोगों को दंडित कर सकती हैं। लेकिन ट्रेलर के दृश्यों के आधार पर अदालत का विचार, जिसमें एक जज को दिखाया गया है, न्यायपालिका का अनादर किया गया है, स्पष्ट रूप से गलत है। जब किसी फिल्म की बात आती है, तो हम सभी जानते हैं कि इसके पात्र, स्क्रिप्ट काल्पनिक और हास्यप्रद हैं, और सच्चाई नहीं। फिल्म के जरिए लोगों की भावनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। इसे कल्पना के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि इसकी वास्तविकता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधान प्रदान करते हैं कि प्रमाणित करने के लिए, सेंसर, सुझाव अधिकार सीबीएफसी की शक्ति है, इस अधिनियम में कहीं भी प्रमाणन प्रक्रिया में न्यायिक, अदालत द्वारा नियुक्त समिति की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है।
जब अदालत ने सीबीएफसी को यह आदेश दिया, तो यह एक असमान हस्तक्षेप था और इसे न्यायिक अतिरेक कहा जाएगा क्योंकि यह न्यायपालिका का काम नहीं है। इसके अलावा, न्यायालय का आदेश अनुच्छेद 19 (2) का उल्लंघन है क्योंकि यह केवल विधिवत अधिनियमित कानून द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, जो कि न्यायालय का आदेश नहीं हो सकता था। ऐसा ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जॉली एलएलबी 1 में आया जब कोर्ट ने कहा कि इसमें जनहित जैसा कुछ नहीं है और ट्रेलर के आधार पर ही फैसला करना गलत होगा। जब आमिर खान की फिल्म पीके के खिलाफ याचिका दायर की गई तो जस्टिस लोढ़ा ने कहा कि “अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो इसे न देखें। भारत एक परिपक्व समाज है और यहाँ के लोग मनोरंजन और अन्य चीजों के बीच का अंतर जानते हैं।”
इसके अलावा, श्याम नारायण चौकसी बनाम भारत संघ के मामले में, माननीय अदालत ने राष्ट्रगान की देशभक्ति को लागू करते हुए फिल्म शुरू करने से पहले सिनेमाघरों में इसे बजाना अनिवार्य कर दिया था। इसने लोगों के लिए खड़ा होना भी अनिवार्य कर दिया, इस आदेश के साथ की सभी दरवाजे बंद रहेंगे, और राष्ट्रीय ध्वज को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जायगा। अदालत का यह जनादेश एक न्यायिक अतिरेक है क्योंकि यह एक दिशानिर्देश है, जिसके पीछे कोई कानून नहीं है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम (प्रिवेंशन ऑफ़ इंसलटस टू नेशनल ऑनर एक्ट), 1971 में कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर राष्ट्रगान के गीतों को रोकता है, उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन इस कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर इसे बजाना अनिवार्य है। बिजो इमैनुएल के मामले में, अदालत ने कहा कि एक इंसान के लिए एक व्यक्तिगत धार्मिक कारण हो सकता है कि वह राष्ट्रगान नहीं गा सकता है या शारीरिक अक्षमता के कारण खड़ा नहीं हो सकता है। अतः इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रगान को अनिवार्य रूप से करना और स्थापित न्यायिक मिसाल के विरुद्ध करना गलत है।
स्टेट ऑफ़ तमिलनाडु बनाम के. बालू के मामले में, सर्वोच्च न्यायलय ने सड़क सुरक्षा के लिए एक याचिका पर विचार करते हुए, किसी भी राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग के 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, ताकि राजमार्ग उपयोगकर्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। निर्णय लोगों की बेहतरी के लिए अनुच्छेद 47 के कार्यान्वयन, सड़क दुर्घटनाओं की खतरनाक संख्या सहित विभिन्न कारणों पर आधारित था। इस मामले में, अदालत ने एक नीति स्थापित करने के मूल्य को समझने के लिए संघर्ष किया जिसे किसी भी स्थिति में लागू किया जा सकता था और किसी प्रकार के परीक्षण पर आधारित था ताकि इसे भविष्य में एक मिसाल या दिशानिर्देश के रूप में माना जा सके। अदालत को इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि क्या किसी तरह का दबाव था जिसके कारण उसने यह फैसला सुनाया। प्रतिबंध निस्संदेह परेशानी भरा था, क्योंकि कुछ सरकारों ने लगाए गए प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप राजस्व हानि से बचने के लिए राज्य के राजमार्गों का नाम बदलकर मुख्य शहर की सड़कों पर करना शुरू कर दिया था। इस मामले में अदालत की मंशा सड़क हादसों को कम करने के लिए सक्रिय थी, लेकिन अदालत ने इसे रोकने के लिए सरकारों को कुछ आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह देने के बजाय, बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की है।
हाल ही में, जब आंध्र प्रदेश में आपातकाल लगाया गया था, उस समय उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबीअस कार्पस) का मामला दायर किया गया था, जिसके दौरान अदालत ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक जांच इस विषय पर थी कि क्या राज्य में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार में “संवैधानिक टूटना (कोंस्टीटूशनल ब्रेकडाउन)” है। यह देखने की शक्ति कि क्या किसी राज्य में संवैधानिक टूटना है, अनुच्छेद 356 के दायरे में कार्यपालिका के पास है, और यदि ऐसा है, तो यह कार्यपालिका की शक्ति है कि वह इसे लागू करे और न कि न्यायपालिका। एसआर बोम्मई मामले से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायपालिका की भूमिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की घोषणा के बाद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आपातकाल लगाया है और उद्देश्य की स्थिति मौजूद है या नहीं, लेकिन जब कोर्ट ने मौजूदा मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया, तो उसने अपनी सीमा का उल्लंघन किया और एक कार्यकारी के रूप में काम किया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और इसे न्यायिक अतिक्रमण करार कर दिया।
भारत में न्यायिक अतिरेक का प्रभाव
इन विभिन्न हाल के उदाहरणों को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि न्यायिक अतिरेक द्वारा अपने कार्य को करने में विधायिका पिछड़ रही है, जिससे न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष हो रहा है, जो लोकतंत्र के साथ-साथ शक्तियों के पृथक्करण के लिए भी हानिकारक है। न्यायिक अतिरेक के विभिन्न प्रभाव हैं जिन्हें नीचे देखा जा सकता है: –
- यह लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक भावना को कमजोर करता है, क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के लिए एक खतरा है। यह सरकार की विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच एक फूट का कारण बनता है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप, जनता के लिए विधायी निष्क्रियता की धारणा है। न्यायपालिका सकारात्मक सक्रियता के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रयोग तब कर सकती है जब कानून में कोई कमी या खामियां हों और अदालत इसे भर सकती है, जब कोई कानून नहीं है या विधायिका लागू करने में विफल रहती है, लेकिन न्यायिक अतिरेक से यह केवल सामाजिक बाधा उत्पन्न कर सकती है कल्याण या अन्य शाखाओं के अधिकार को कमजोर करता है।
- कुछ स्थितियों में, प्रभावी ढंग से समझने और काम करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, पर्यावरण, आर्थिक और विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए, ऐसे परिदृश्य में, यदि न्यायपालिका अपनी सीमा से परे जाती है और इस मुद्दे के साथ कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद निर्णय देती है, तो यह देश के लिए हानिकारक है और नुकसान का कारण बनता है, जैसा कि शराब प्रतिबंध के उदाहरण में देखा गया है।
- एक तरफ न्यायिक सक्रियता है, जो लोगों को न्यायिक प्रणाली पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह विश्वास कराते हुए कि अगर उनके साथ या समाज में कुछ भी अनुचित है, तो अदालत उनके सर्वोत्तम हित में ही कार्य करेगी। दूसरी ओर, न्यायिक अतिरेक दर्शाता है कि वैकल्पिक प्रतिनिधित्व (इलेक्टिव रिप्रजेंटेशन) के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए अदालत अपने तरीके से चलेगी। यह लोकतांत्रिक संस्थानों में लोगों के विश्वास को मिटा देगा और अंततः उन मामलों को तय करने वाले न्यायाधीशों को स्वायत्तता (ऑटोनोमी) देकर लोकतंत्र को नष्ट कर देगा जो न्यायपालिका के क्षेत्र में भी नहीं आते हैं।
- कानून के शासन की अवधारणा कानून की सर्वोच्चता बताती है लेकिन न्यायिक अतिरेक में अदालत के शासन का उल्लेख है कि, अदालत का फैसला कानून के लिए सर्वोच्च है, जो शक्तियों के पृथक्करण का एक स्पष्ट उल्लंघन है। न्यायपालिका नीति नहीं बनाती; बल्कि, वे इसकी वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करते हैं, जो ऐसा करने की प्रवृत्ति होने पर घबराहट पैदा कर सकता है। इसलिए, न्यायपालिका का दायित्व है कि वह अन्य शाखाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचे।
सर्वोच्च न्यायलय, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से भारतीय नागरिकों के जीवन के कई दैनिक पहलुओं को प्रभावित करने में सक्रिय रहा है, लेकिन न्यायिक अतिरेक की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और अदालत को प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के आधार पर अपने अति सक्रिय दृष्टिकोण को सही ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं यह कहते हुए सीमा निर्धारित की है कि, “अधिक सक्रिय दृष्टिकोण से बचने के लिए न्यायाधीशों पर विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे राज्य की अन्य दो शाखाओं के लिए निर्धारित क्षेत्रों के भीतर अतिचार नहीं करते हैं” और जानबूझकर इसका पालन करना चाहिए।
न्यायिक जवाबदेही (जुडिशियल एकाउंटेबिलिटी)
इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली का अविश्वसनीय महत्व और अधिकार है। हालाँकि, प्राधिकरण एक कीमत पर आता है, इसमें बहुत अधिक जवाबदेही होती है और नियमों और विनियमों के कठोर अनुपालन की आवश्यकता भी होती है। न्यायपालिका के व्यापक अधिकार से न्यायाधीशों के मन में अधिकार के दुरुपयोग का डर पैदा होता है। हालांकि, संविधान समय के साथ नियंत्रण और संतुलन प्रणाली को नष्ट करते हुए न्यायपालिका को किसी के प्रति जवाबदेह ठहराने में विफल रहता है।
भारत में, कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की जाती है, जब कोई अन्याय होता है, विधायिका के कार्यों की भी उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाती है यदि वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून बनाता है और यदि कोई मनमानी करता है। लेकिन, न्यायिक प्रणाली के मामले में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूसरे अंग को अपने फैसलों पर रोक लगाने में सक्षम बनाता है, केवल उच्च बेंच ही हस्तक्षेप और निर्णय ले सकती है। नतीजतन, न्यायाधीशों को न केवल उनके व्यक्तिगत कार्यों और क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, साथ ही साथ उनके द्वारा सुनाए गए कानूनी निर्णयों के लिए, जो अक्सर भ्रमित करने के लिए होते हैं। न्यायिक जवाबदेही की अनिवार्यता और भी जरूरी हो गई है क्योंकि अदालतें अब न केवल न्यायिक बल्कि अर्ध-कार्यकारी भूमिकाएं भी निभाती हैं, जिसके लिए कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह होती है।
निष्कर्ष
भारत में, न्यायिक प्रणाली में अपने संवैधानिक क्षेत्र से बाहर भटकने की प्रवृत्ति है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक प्रयोग होता है, जिसे हमेशा कानूनी नहीं माना जा सकता है। यद्यपि भारत में शक्तियों के कठोर पृथक्करण का नियम पहले से ही काफी प्रभावी है, लेकिन न्यायपालिका अक्सर ऐसे विवादों का निर्णय करते समय न्यायिक संयम का प्रयोग नहीं करती है जो राजनीतिक हैं या व्यापक सार्वजनिक निहितार्थ (इम्प्लीकेशन) हैं। न्यायाधीश उन जटिल विषयों पर भी राय व्यक्त करते हैं जो उनके दायरे से बाहर हैं, और प्रमुख नीतिगत चिंताओं पर जो विधायिका और कार्यकारी अधिकारियों के विशेषाधिकार हैं।
उपर दिए गए विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सक्रियता के साथ कार्यपालिका और विधायिका के अनैतिक और असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ समाज के वंचित लोगों की रक्षा की है, लेकिन यह अपनी सीमा को भी पार कर गया है। अदालत ने विभिन्न मामलों में उस क्षेत्र में काम करने के अपने दायित्व को समझा है जहां विधायिका और कार्यपालिका की ओर से कानून या विफलता है। लेकिन, विभिन्न मामलों में यह इन शाखाओं की गतिविधियों को परेशान करते हुए इनके क्षेत्र में पहुंच गया है। अदालत ने हमेशा हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल किया है, लेकिन न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायाधीश बिना औचित्य के प्रशासनिक या विधायी भूमिका निभाने का प्रयास नहीं करते हैं। अब, न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता है क्योंकि जब न्यायपालिका अधिकता का दोषी है, केवल एक बड़ी बेंच या संशोधन ही इसमें हस्तक्षेप कर सकता है।
भारतीय संविधान सरकार को तीन शाखाओं में विभाजित करता है, जिनमें से किसी को भी पूर्ण नियंत्रण या अधिकार प्राप्त नहीं है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि शायद सरकार की एक शाखा में सत्ता का संकेंद्रण (कंसंट्रेशन) लोकतंत्र की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। नतीजतन, न्यायिक सरलता का इस्तेमाल संविधान को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है और न्यायपालिका को इसकी सीमा से अधिक होने से रोकने की आवश्यकता है।
संदर्भ
-
- Kanishka Sihare, Judicial Review and Judicial Over-reach: Transition of Scenario, Lawsisto (Dec. 10, 2019), https://lawsisto.com/artcileread/MzQ3/JUDICIAL-REVIEW-AND-JUDICIAL-OVER-REACH-TRANSITION-OF-SCENARIO.
- Constituent Assembly Debates, Volume VIII, May 24, 1949, Constitution of India, https://www.constitutionofindia.net/constitution_assembly_debates/volume/8/1949-05-24
- Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803).
- R Shunmugasundaram, Judicial activism and overreach in India, 72 Amicus Curiae – Journal of the Society for Advanced Legal Studies 22, 22 (2007).
- Shankari Prasad v. Union of India, AIR 1951 SC 458.
- Indira Gandhi v. Raj Narain, AIR 1975 SC 2299.
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461.
- Sajjan Singh v. State of Rajasthan, AIR 1965 SC 845.
- Minerva Mills v. Union of India, AIR 1980 SC 1789.
- L. Chandra Kumar v. Union of India, AIR 1997 SC 1125.
- Yeshwant Naik, Homosexuality in the Jurisprudence of the Supreme Court of India 68 (Springer International Publishing 2017).
- B Nagarathnam Reddy, Judicial Activism vs Judicial Overreach in India, 7(1) GJRA – Global Journal for Research Analysis 82 (2018).
- Md. Mostafizur Rahman & Roshna Zahan Badhon, A Critical Analysis on Judicial Activism and Overreach, 23(8)(3) IOSR Journal of Humanities and Social Science 45 (2018).
- Black’s Law Dictionary 922 (9th ed. 2009).
- Swati Sharma, Rahul Rishi & M. S. Ananth, Judicial Activism in India: Whether more Populist or Less Legal?, 1(1) Indian Journal of Constitutional & Administrative Law 11 (2017).
- Anil Kumar Dubey, Legislative Role of Judiciary in India: A Critical Appraisal, ILI Law Review (Summer Issue 2019).
- Dr. Manmohan Singh – Speech, PM’s address at the Conference of Chief Ministers & Chief Justices of High Courts, Archivepmo (Apr. 08, 2007), https://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=502.
- Today’s Paper, Don’ cross limits, apex court asks judges, The Hindu (Dec. 11, 2007), https://www.thehindu.com/todays-paper/Donrsquot-cross-limits-apex-court-asks-judges/article14892761.ece.
- Archive, Judicial activism should be neither judicial ad hocism nor judicial tyranny, The Indian Express (Apr. 05, 2007, 23:58 IST), http://archive.indianexpress.com/news/-judicial-activism-should-be-neither-judicial-ad-hocism-nor-judicial-tyranny-/27579/5.
- Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, (1997) 10 SCC 549.
- Neeraja Chaudahary v. Union of India, AIR 1984 SC 1099.
- People’s Union for Democratic Rights v. Union of India, (1983) 1 SCC 525.
- M. C. Mehta v. State of Tamil Nadu, (1996) 6 SCC 756.
- Sheela Barse v. Union of India, (1986) 3 SCC 596.
- Gaurav Jain v. Union of India, AIR 1997 SC 3021.
- Lakshmi Kant Pandey v. Union of India, AIR 1984 SC 469.
- Vishakha v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011.
- Lakshmi Muralidhar, The Judiciary on its Over-reach, 1(3) International Journal of Law Management & Humanities 1 (2018); R Shunmugasundaram, Judicial activism and overreach in India, 72 Amicus Curiae – Journal of the Society for Advanced Legal Studies 22, 27 (2007).
- Dr. Maneesh Yadav, Judicial Activism, Prison Management and Prisoners’ Rights in India: An Analysis, 7(14) Journal of Critical Reviews 714 (2020).
- Joginder Kumar v. State of U.P., AIR 1994 SC 1349.
- People’s Union for Civil Liberties v. Union of India, AIR 1997 SC 1203.
- D. K. Basu v. State of West Bengal, AIR 1997 SC 610.
- Sunil Batra v. Delhi Administration, (1978) 4 SCC 409.
- Hussanaira Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar, AIR 1979 SC 1360.
- Inder Singh v. The State (Delhi Admn.), AIR 1978 SC 1091.
- Murli S. Deora v. Union of India, (2001) 8 SCC 765.
- Ajaykumar v. Union of India, 2017 SCC OnLine Bom 126.
- Vrinda Bhandari, Courts and contempt powers in India: The case of Jolly LLB-2, Oxford Human Rights Hub – Blog (Apr. 04, 2017), http://ohrh.law.ox.ac.uk/courts-and-contempt-powers-in-india-the-case-of-jolly-llb-2/.
- FPJ Bureau, SC on Aamir film ‘PK’ ‘If you don’t like it, don’t watch it’, The Free Press Journal (Aug. 15, 2014, 01:01 AM), https://www.freepressjournal.in/headlines/sc-on-aamir-film-pk-if-you-dont-like-it-dont-watch-it.
- Shyam Narayan Chouksey v. Union of India, AIR 2018 SC 357.
- Bijoe Emmanuel v. State of Kerala, AIR 1987 SC 748.
- Apar Gupta, A legal overdose of patriotism, Live Mint (Dec. 02, 2016, 04:58 AM), https://www.livemint.com/Opinion/yGaPvap9RAMNcRbZzAO6CJ/A-legal-overdose-of-patriotism.html.
- State of Tamil Nadu v. K. Balu, (2017) 2 SCC 281.
- Satyam Tandon, Case Comment: The Highway Liquor Ban Case: State of Tamil Nadu v. K. Balu & Others, 6(2) Christ University Law Journal 77 (2017).
- S. R. Bommai v. Union of India, AIR 1994 SC 1918.
- Editorial, The right call: On A.P. High Court order, The Hindu (Dec. 21, 2020, 00:39), https://www.thehindu.com/opinion/editorial/the-right-call-on-ap-high-court-order/article33379622.ece.
- Supriyo Ranjan, Judicial Activism – Is it Justified?, Manupatra, http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/4BBA6619-936F-436A-BDF3-ADB893D38B6A.pdf.
- State of Kerala v. A. Lakshmikutty, (1986) 4 SCC 632 at 657.
- Divyanshu Bahndari & Vaibhav Patel, Judicial Accountability and the Independence of The Indian Judiciary, 2(7) International Journal of Liberal Arts and Social Science 144 (2014).
- Isha Tirkey, CCS Working Paper No. 247 – Judicial Accountability in India: Understanding and Exploring the Failures and Solutions to Accountability, Centre for Civil Society (2011), https://ccs.in/internship_papers/2011/247_judicial-accountablity-in-india_isha-tirkey.pdf.