यह लेख नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा की कानून की छात्रा Ansruta Debnath ने लिखा है। यह लेख आच्छादन के सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ एक्लिप्स) के बारे में बात करता है जो एक कानूनी सिद्धांत है जिसका उपयोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पूर्व-संवैधानिक कानूनों को मान्य करने के लिए किया गया है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारतीय कानूनों के तहत आच्छादन का सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि कोई भी मौजूदा कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, वह पूरी तरह से अमान्य नहीं होता है। इसे वैध बनाया जा सकता है यदि भारत के संविधान, 1950 में उपयुक्त संशोधन (अमेंडमेंट) किए जाते हैं, जिससे उस कानून का तालमेल मौलिक अधिकारों के साथ बिठाया जा सके। यह सिद्धांत इस आधार पर टिका है कि मौलिक अधिकार संभावित हैं। इस प्रकार, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी पूर्व-संवैधानिक कानून शून्य नहीं होगा क्योंकि उस कानून के निर्माण के समय, भारत के संविधान, 1950 के मौलिक अधिकार अस्तित्व में नहीं थे। हालाँकि, सवाल उठे हैं कि क्या यह सिद्धांत संवैधानिक कानूनों के बाद भी लागू होता है, जो इस लेख में संबोधित किया गया है।
आच्छादन का सिद्धांत और भारतीय संविधान
यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित है जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अपमानजनक कानूनों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर संविधान के प्रारंभ से पहले, लागू कोई भी मौजूदा कानून जो भारतीय संविधान के भाग III में मौजूद मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है या असंगत (इनकंसिस्टेंट) है, तो वह ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य हो जाता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि कोई भी नया कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सीमा तक, इस तरह के उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाता है। ये प्रावधान सीधे तौर पर पृथक्करणीयता (सेवरेबिलिटी) के सिद्धांत के अनुरूप हैं। यह सिद्धांत बताता है कि किसी क़ानून का कोई भी प्रावधान जो संविधान के विरुद्ध है, उसे उस अधिनियम से अलग कर दिया जाएगा और केवल उस सीमा तक ही शून्य माना जाएगा। इस प्रकार, न्यायालयें पूरे अधिनियम के बजाय उस प्रावधान को शून्य घोषित कर सकती हैं। हालांकि, अनुच्छेद 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 13 संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन कानून पास हो जाता है जो कुछ मौलिक अधिकारों को छीन लेता है या उनका उल्लंघन करता है, तो वे कानून, हालांकि जो अधिकारों से असंगत हैं, वह शून्य नहीं हैं।
आच्छादन के सिद्धांत की उत्पत्ति और विकास
भारतीय संविधान के लागू होने के बाद, कई मौजूदा कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती थी। इसी तरह, न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) ने आच्छादन के सिद्धांत को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जबकि भीकाजी नारायण धाकरा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) वह मामला था जहां इस कानूनी सिद्धांत को औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा घोषित किया गया था, इस सिद्धांत का इस्तेमाल कुछ अन्य पिछले मामलों में मुख्य रूप में किया गया था।
पहला मामला जहां इस सिद्धांत की उत्पत्ति के निशान पाए जा सकते हैं वह है केशव मदवन मेनन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे (1951)। इस मामले में, अपीलकर्ता के खिलाफ 1949 में प्रकाशित एक पैम्फलेट के संबंध में भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931 के तहत खुद के खिलाफ मामला था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ ऐसा मामला नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह पैम्फलेट में दी गई सही वाक् और अभिव्यक्ति (स्पीच एंड एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के साथ संरेखित (अलाइन्ड) है। न्यायालय ने कहा कि क्योंकि जिस समय पैम्फलेट प्रकाशित हुआ था, उस समय भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार मौजूद नहीं थे। इस प्रकार, अपीलकर्ता उनके पास होने का दावा नहीं कर सकता था। इस प्रकार इस मामले ने स्थापित किया कि मौलिक अधिकारों का पूर्वव्यापी प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) नहीं था, बल्कि केवल भावी अनुप्रयोग (प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन) था। अनुच्छेद 13(1) के मामले में, न्यायालय ने माना कि यह संभावित था और पूर्वव्यापी नहीं था, खासकर जब से कोई क़ानून संभावित है, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो। चूँकि इस अनुच्छेद की भाषा किसी भी प्रकार के पूर्वव्यापी आवेदन का संकेत नहीं देती है, इसलिए इसे आच्छादन नहीं किया जा सकता है। इस मत को पन्नाला बिनाराज बनाम भारत संघ (1957) के मामले में दोहराया गया था।
अगला महत्वपूर्ण मामला, जिसमें अनुच्छेद 13(1) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पूर्व-संवैधानिक कानूनों के बीच के संबंध के बारे में बात की गई थी, वह बेहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम बॉम्बे राज्य (1955) का मामला था। इसमें, अपीलकर्ता पर मुंबई दारुबंदी अधिनियम, 1949 की धारा 66 (B) के तहत आरोप लगाया गया था। इस धारा में शराब के प्रभाव में ड्राइविंग के बारे में बताया गया था। अपीलकर्ता ने बॉम्बे राज्य और एनआर बनाम एफएन बलसारा (1951) के मामले का इस्तेमाल किया, जहां अधिनियम की धारा 13 (B) को मादक औषधीय और शौचालय की तैयारी के उपयोग के लिए इसके आवेदन की सीमा तक शून्य घोषित किया गया था क्योंकि वही अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) द्वारा, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 66 (B) को भी शून्य माना जाना चाहिए क्योंकि उसमे मादक औषधीय और शौचालय में इस्तेमाल की जाने वाली औषधि का संबंध था।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने शुरू में माना कि बलसारा मामले ने धारा को निरस्त (रिपील) या संशोधित नहीं किया। लेकिन एक बड़ी संवैधानिक पीठ के संदर्भ में, बहुमत की राय ने माना कि नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के लिए धारा को क़ानून से “काल्पनिक रूप से मिटा दिया गया” था। आगे यह माना गया कि बलसारा में फैसला मादक औषधीय और शौचालय में इस्तेमाल की जाने वाली औषधि के संबंध में धारा 66 (B) के तहत एक आरोप के लिए एक अच्छा बचाव था। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि आरोपी मादक औषधि बनाने के अलावा किसी भी प्रतिबंधित शराब के प्रभाव में गाड़ी चला रहा था और आरोपी को इसी के विपरीत साबित करना था।
भीकाजी नारायण धाकरा बनाम मध्य प्रदेश राज्य
सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आच्छादन के सिद्धांत को स्पष्ट और प्रतिपादित (प्रोपाउंड) करने के लिए जिम्मेदार था, वह भीकाजी नारायण धाकरा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) का मामला था। इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने सीपी और बरार मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1947 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, जिसने मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन किया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के पारित होने से संशोधन अधिनियम शून्य हो गया क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करता है या किसी पेशे का अभ्यास (प्रैक्टिस) करने या कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संशोधन ने प्रांतीय सरकार को राज्य में मोटर परिवहन (ट्रांसपोर्ट) व्यवसाय पर एकाधिकार (मोनोपॉली) स्थापित करने की अनुमति दी थी, जिसे याचिकाकर्ताओं ने 1950 के नवनिर्मित भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था।
उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि यद्यपि अधिनियम प्रारंभ में भारतीय संविधान का उल्लंघन था, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 और संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 के पास होने के बाद, अनुच्छेद 19(6) के अतिरिक्त के माध्यम से विसंगतियों (इनकंसिस्टेंसी) को हटा दिया गया था और सीपी और बरार मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम फिर से लागू किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिक्रिया में स्पष्ट रूप से कहा कि यह अधिनियम अनुच्छेद 13(1) के अनुसार शून्य हो गया था और जब तक कि उसे दोबारा अधिनियमित नहीं किया गया तब तक वह अस्तित्व में नहीं है ऐसा माना गया था।
हालांकि याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादियों के तर्कों को स्वीकार कर लिया गया था। भीकाजी मामले के फैसले से कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं-
- शुरुआत के लिए, निर्णय केशव मामले पर निर्भर था। इसके अलावा, यह कहा गया है कि अनुच्छेद 13 में “शून्य” शब्द का अर्थ मौलिक अधिकारों के साथ असंगति की सीमा तक ही शून्य है।
- इसका मतलब यह हुआ कि अधिनियम का पूरा संचालन (ऑपरेशन) बंद नहीं हुआ था। अनुच्छेद 13 (1) को एक मौलिक अधिकार के साथ असंगत, असंगतता की सीमा तक निष्क्रिय (इनैक्टिव) अधिनियम प्रस्तुत करना था। यह मौलिक अधिकार से ढका हुआ है और निष्क्रिय रहता है लेकिन मृत नहीं होता है।
- यह आच्छादन का सिद्धांत है। मौलिक अधिकार के साथ असंगति, अधिनियम को तब तक आच्छादन करती है जब तक असंगति है, इसलिए आच्छादन को हटाया नहीं जाता है।
- संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 और अनुच्छेद 19 के खंड (क्लॉज) 6 में परिवर्तन के साथ, आक्षेपित (ऑब्जेक्टेड) अधिनियम के प्रावधान अब असंगत नहीं थे और इसका परिणाम यह हुआ कि इस तरह के संशोधन की तारीख से अधिनियम एक बार फिर से लागू होना शुरू हो गया था।
भारतीय दंड संहिता में आच्छादन के सिद्धांत को लागू करना
पी. राठीराम बनाम भारत संघ (1994) के मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 309, जो आत्महत्या करने के प्रयासों को दंडित करती है, उसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था। यह फैसला सुनाया गया था कि धारा 309 अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है जो बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ न बोलने का अधिकार भी देता है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि यह धारा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है जो कि बहिर्वेशन (एक्स्ट्रापोलेशन) द्वारा भी नहीं जीने का अधिकार देती है।
इसे जियान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996) में एक अमान्य खोज (इनवैलिड फाइंडिंग) माना गया था। इस प्रकार, संक्षेप में, राठीराम मामले ने मौलिक अधिकारों के साथ धारा 309 को आच्छादन कर लिया था जिसे जियान निर्णय द्वारा हटा दिया गया था।
संवैधानिक कानूनों के बाद आच्छादन के सिद्धांत का अनुप्रयोग
जबकि अनुच्छेद 13(1) पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू होता है, अनुच्छेद 13(2) संवैधानिक कानूनों के बाद लागू होता है। इन दो खंडों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर दीप चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959) में तैयार किया गया था। यहां, यह कहा गया था कि भारतीय संविधान के भाग III द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ विसंगतियों की सीमा को छोड़कर भाग lll एक पूर्व-संवैधानिक अस्तित्व में है, लेकिन भाग III के उल्लंघन में कोई भी पूर्व-संवैधानिक कानून नहीं बनाया जा सकता है और यदि बनाया गया है तो वह शुरुआत से शून्य है। इस प्रकार, अनुच्छेद 13 को पढ़ने से, आच्छादन का सिद्धांत संवैधानिक कानूनों के बाद लागू नहीं हो सकता है। सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1954) में, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि जो अधिनियम भारतीय संविधान के प्रारंभ के बाद अधिनियमित हुए है और अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करते हुए खंड 6 द्वारा संरक्षित नहीं किए गए है ऐसे किसी भी कानून को वैध नहीं बनाया जा सकता है।
इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण मामला महेंद्र लाई जैनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963) है। इस मामले में, यह आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया था कि आच्छादन का सिद्धांत संवैधानिक कानूनों के बाद लागू नहीं होता है और बाद में संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्वचालित (ऑटोमैटिक) रूप से पुनर्जीवित (रिवाइव) नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसा कि अनुच्छेद 13(2) में दिया गया है, तो आक्षेपित अधिनियम प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगा। उस क़ानून को लागू करने के लिए, संविधान में संशोधन करना होगा और पहले वाले को फिर से अधिनियमित करना होगा। इस सिद्धांत को के के पूनाचा बनाम कर्नाटक राज्य (2010) में दोहराया गया था। इस मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या किसी अधिनियम को इस आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं था और संविधान के अनुच्छेद 31 (3) की आवश्यकता के अनुसार उसकी सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। यह माना गया कि एक अधिनियम सिर्फ इसलिए रद्द नहीं हो जाता क्योंकि उसे सहमति नहीं मिली थी। जब तक अनियमितता दूर नहीं हुई तब तक यह आच्छादन लगा रहता है। वर्तमान परिदृश्य (सिनेरियो) में, अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार, अधिनियम फिर से पुनर्जीवित हो गया था।
इस सिद्धांत का उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी किया गया है। उदाहरण के लिए, के पी मनु, मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, स्क्रूटनी कमेटी (2015) के मामले में, न्यायालय ने कहा कि जब कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो मूल जाति आच्छादन के अधीन रहती है और जैसे ही उसके जीवनकाल में व्यक्ति मूल धर्म में वापस आ जाता है, आच्छादन गायब हो जाता है और जाति स्वतः पुनर्जीवित हो जाती है। इसके अलावा, यूओआई और अन्य बनाम दुली चंद (2010) के मामले में, न्यायालय ने माना कि रोके जाने पर शिक्षा के आदेश को आच्छादन किया जाएगा और वह मृत नहीं होगा। जब उसी रुकावट को निकाल दिया जाता है, तो उसी क्षण से, उसकी उर्वरित शिक्षा फिर से शुरू हो जाएगी।
निष्कर्ष
इस प्रकार, आच्छादन के सिद्धांत का अनुप्रयोग बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि यह संवैधानिक संशोधनों की अनुमति देकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले पूर्व-संवैधानिक कानूनों को मान्य कर सकता है, वह संवैधानिक कानूनों के बाद लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्व और बाद के संवैधानिक कानूनों के मुद्दे, अनुच्छेद 13 के तहत अलग-अलग हैं। पूर्व-संवैधानिक कानूनों के संबंध में, यह सिद्धांत असंवैधानिक कानूनों को निष्क्रिय बनाकर असाधारण परिस्थितियों में उनको मिटाए जाने से बचाने की अनुमति देता है जब तक कि उन्हें भविष्य में पुनर्जीवित नहीं किया जाता है।
संदर्भ
- आच्छादन का सिद्धांत – CuriousForLaw


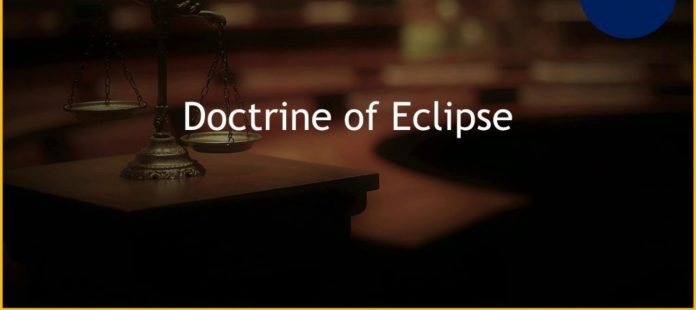
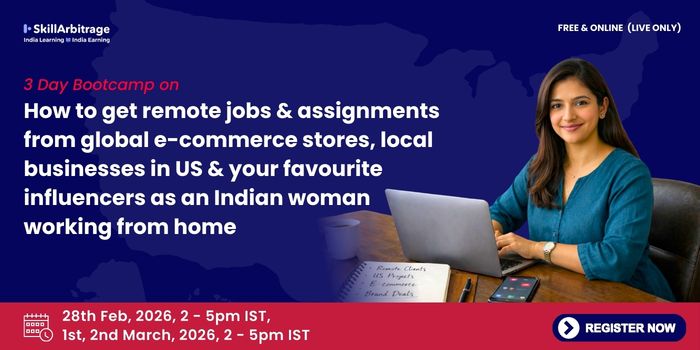





Good nice collection . Koi respo.jab lower court me anupasthit hokar ek pakshi ho jata hai .kya use appeal mein Samman karna avashyak hai.