यह लेख Indrasish Majumdar, द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो के एक इंटर्न है। इस लेख को Ruchika Mohapatra (एसोसिएट, लॉसिखो) और Arundhati Das (लॉसिखो में इंटर्न) द्वारा एडिट किया गया है। इस लेख में उन्होंने हिन्दू कानून के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा के सिद्धांत पर चर्चा की है और साथ ही संवैधानिक कानून और व्यक्तिगत कानून का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। एक इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
सामान्य अवलोकन (ओवरव्यू)
भारत में धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) का सिद्धांत काफी सरल है। हालाँकि शुरू में धार्मिक विश्वास के अभ्यास और प्रसार (स्प्रेड) को राज्य के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया गया था, उपनिवेशवाद (कॉलोनियलिज्म) के बाद के भारत में धर्मनिरपेक्षता, इसकी पश्चिमी परंपरा के इतिहास से दोहराया गया सिद्धांत नहीं था। भारत में धर्मनिरपेक्षता बहुत भिन्न थी, क्योंकि भारत के कई धार्मिक समुदायों की जटिलता के अलावा, उसे अपने लोगों की विशिष्ट सामाजिक-धार्मिक सांस्कृतिक पहचान को शामिल करना था। अनिवार्य रूप से, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के तीन पहलू हैं:
- धर्म, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों में कभी भी कोई भूमिका नहीं निभाएगा;
- राज्य के गैर-हस्तक्षेपवादी (नॉन इंटरवेंशनिस्ट) आकृति से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह यह गारंटी देकर धर्म की समान स्वतंत्रता प्रदान करेगा कि यह व्यक्ति और उसके धार्मिक विश्वास के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- सरकारी हस्तक्षेप, धर्म के दायरे की पुनर्व्याख्या (रीइंटरप्रेट) करने के लिए था, जबकि राज्य से गैर-हस्तक्षेप, धार्मिक प्रतिष्ठानों (एस्टेब्लिशमेंट) को राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता प्रदान करना था।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय, धर्म और संविधान के बीच संबंध को निर्धारित करने के लिए एक प्रमुख सिद्धांत के साथ आया था। यह सिद्धांत बताता है कि यदि कोई प्रथा किसी विशिष्ट धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, तो सरकार द्वारा इसकी निगरानी या इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्ताव बाद में “आवश्यक धार्मिक प्रथा के परीक्षण” में रूपांतरित (मॉर्फ्ड) होने के मूल में था। परीक्षण ने अदालतों को दो दृष्टिकोणों के साथ छोड़ दिया – पहला, जिसमें धर्म द्वारा ही यह तय किया गया था कि इसकी पवित्र पुस्तकों और शिलालेखों (इंस्क्रिप्शंस) के बाद क्या आवश्यक है और क्या नहीं। दूसरा यह था कि अदालतें सांस्कृतिक आलोचक की भूमिका निभाएं और भारत में जीवन के धार्मिक क्षेत्रों को अस्थायी लोगों से अलग करें।” आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का परीक्षण” का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहली बार आयुक्त (कमिश्नर), हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (एंडोमेंट), मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, के मामले में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि धर्म की स्वतंत्रता को संविधान में प्रतिष्ठापित (इनश्राइन) किया गया था और यह धार्मिक प्रथाओं तक विस्तारित है और केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं था, और संविधान के तहत सीमाओं के अधीन था।
सर्वोच्च न्यायालय दो दृष्टिकोणों के बीच अस्पष्ट थे और उन दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण को अभी तक, निश्चित रूप से नहीं अपनाया गया है। कई मामले धर्म पर एक विशेष मानदंड (नॉर्म) की अनिवार्यता को निर्धारित करने की जिम्मेदारी डालते हैं, जबकि अन्य उस जिम्मेदारी को अदालतों पर रखते हैं। पहले दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि धार्मिक समूह अनुचित रूप से प्रत्येक कार्य/ प्रथा को ‘आवश्यक’ के रूप में मान सकते हैं, जो किसी भी विधायी सुधार के लिए बहुत कम गुंजाइश प्रदान करता है। यह धर्म के आधार पर विभाजनकारी लोकलुभावनवाद (डिविसिव पॉपुलिज्म) को बढ़ावा देता है, क्योंकि असंगठित समूह धार्मिक आख्यानों (नैरेटिव्स) द्वारा समर्थित राजनीतिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। बाद के दृष्टिकोण के साथ, इस बात पर विचार किया जाता है कि धार्मिक क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन पर निर्णय लेने के लिए अदालतें उपयुक्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि भारत में धार्मिक पहलू अक्सर नीति-संबंधी मुद्दों की ओर होते हैं।
इस लेख का उद्देश्य आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की जांच करना है और यह देखना है की यह कैसे संविधान में निहित पुनरावर्ती (रीपैरेटिव) धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ किसी के धर्म का अभ्यास करने की व्यापक संवैधानिक स्वतंत्रता को एकीकृत करता है। इस लेख का भाग II भारत में पर्याप्त न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) का मूल्यांकन करता है, जो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का परीक्षण करता है और मामलों के माध्यम से विरोधाभासों की पहचान करता है और विवाह और दत्तक (एडॉप्शन) हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत कुछ आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को भी सूचीबद्ध करता है। भाग III ‘आवश्यक’ धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत की आलोचना करता है, इसकी कमियों और समस्याओं पर प्रकाश डालता है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की ख़ासियत को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प का प्रस्ताव करता है। भाग IV भारत में आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के विकल्प को पेश करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए समाप्त होता है।
आवश्यक धार्मिक प्रथा को समझना : कानून और धर्म का मेल
भारत के विविध लोकतांत्रिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, जो नियमों और अधिकारों दोनों की मजबूत नींव पर विकसित हुआ है, केवल कानून और धर्म के दो अलग-अलग क्षेत्रों पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से भिन्न है, यह भी सच है कि कानून और धर्म दोनों ही समाज की मूलभूत आवश्यकताओं का निर्माण करते हैं। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों ने कुछ मानकों को प्रतिपादित (प्रोपाउंड) किया है, जिन्हें धर्म के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण ऐसे विश्वासों की स्थापना और संरक्षण प्रदान करते समय एक बेंचमार्क के रूप में लिया जा सकता है। निम्नलिखित खंडों में, लेखक एक गहन विश्लेषण करते हैं ताकि संवैधानिक कानून के साथ-साथ व्यक्तिगत कानून के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की स्थिति को समझा जा सके।
हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाएं
हिंदुओं के लिए विवाह और दत्तक दो प्रथाएं हैं जिनकी वैधता हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों से ली गई है। इस लेख के निम्नलिखित खंड में दत्तक और विवाह के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानून के तहत कुछ आवश्यक धार्मिक प्रथाओं पर विचार किया जाएगा, जिसके बिना दोनों में से कोई भी प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी नहीं की जा सकती है। “हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5” एक हिंदू विवाह के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में बताती है; अर्थात्: विवाह के समय, कोई भी पक्ष-
- विकृत दिमाग के परिणामस्वरूप वह कानूनी सहमति प्रदान करने में असमर्थ है; या
- भले ही वे बोधित सहमति देने में सक्षम हों, वे प्रकृति की एक मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जो उन्हें शादी और बच्चे पैदा करने के लिए अयोग्य बनाती है; या
- पागलपन के बार-बार कृत्यों से अवगत कराया गया है;
- विवाह के समय दूल्हे की उम्र 21 वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 वर्ष है;
- जब तक प्रथा विवाह की अनुमति नहीं देती तब तक पक्ष निषिद्ध (फोरबिडन) साझेदारी के आदेशों से बाध्य नहीं होती हैं;
- विवाह के पक्षकार तब तक सपिंडा नहीं होते जब तक कि परंपरा द्वारा संबंधित पक्षों के बीच विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है;
- एक दुल्हन को कुंवारी होने की जरूरत नहीं है।
धारा 7 हिंदू विवाह के आवश्यक अनुष्ठानों के बारे मे बात करती है। एक हिंदू विवाह को, संबंधित पक्षों में से किसी एक के पारंपरिक संस्कारों के अनुपालन में मनाया जा सकता है। ऐसा ही एक प्रथागत अनुष्ठान है “सप्तपदी” (दूल्हे और दुल्हन द्वारा एक साथ सात फेरे लेना)। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने “सीमा बनाम अश्विनी कुमार ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 1158” में कहा कि विभिन्न धर्मों से संबंधित सभी भारतीय नागरिकों का वैवाहिक संघ अनिवार्य रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना चाहिए। यदि विवाह का दस्तावेजीकरण किया जाता है, तो अधिकांश वैवाहिक विवादों को सुरक्षित रूप से रोका जा सकता है। पंजीकरण का उद्देश्य महिलाओं के हितों की रक्षा करना और बच्चों के अधिकारों की मान्यता की समस्याओं को रोकना भी था।
“पी रमेश कुमार बनाम सचिव कन्नपुरम ग्राम पंचायत , एआईआर 1998 के.ई.आर 95” के मामले में, केरल उच्च न्यायालय के एकल (सिंगल) न्यायाधीश द्वारा यह राय दी गई थी कि जापानी राष्ट्रीयता वाली एक बौद्ध महिला ने बिना पंजीकरण के एक हिंदू व्यक्ति से विवाह किया था। हालाँकि, पंजीकरण का प्रमाण पत्र विवाह को अमान्य करने की चिंता का विषय नहीं था क्योंकि दूल्हा भारतीय अधिवास नहीं था।
हिंदू शास्त्रों में यह बताया गया था कि हर दत्तक पुत्र को वास्तविक पुत्र के बराबर माना जाना चाहिए। इससे दत्तक पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वह अब केवल एक दत्तक पुत्र ही नहीं था, बल्कि दत्तक परिवार के मातृवंशीय (मैट्रिलिनियल) और पितृवंशीय (पैट्रिलिनियल) पक्ष के सभी संबंधों को प्राकृतिक संबंध माना जाना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि लड़का अपने दत्तक माता-पिता की बेटी से शादी नहीं कर सकता, भले ही बेटी स्वाभाविक रूप से पैदा हुई हो या दत्तक बहन हो। समकालीन दत्तक कानून का मुख्य उद्देश्य एक निःसंतान माता-पिता को आराम और सहायता प्रदान करना है और दूसरी ओर, जरूरतमंद, परित्यक्त (अबैंडन), निराश्रित (डेस्टीट्यूट) या नाजायज बच्चे को माता पिता प्रदान करना है। हालांकि, चंद्रशेखर के मामले में, यह माना गया था कि गोद लेने की वैधता भौतिक (फिजिकल) कारकों के बजाय नैतिक के आधार पर तय की जानी चाहिए और संपत्ति का हस्तांतरण इसलिए माध्यमिक महत्व का होता है।
हिंदू कानून का कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) वर्तमान में “हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, (हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट) 1956” द्वारा विनियमित है, जो केवल हिंदुओं पर लागू होता है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 में निर्दिष्ट है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो धर्म से हिंदू है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्मा, प्रार्थना या आर्य समाज मे मान्यता रखने वाला, या बौद्ध, जैन या सिख” या कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, शामिल हैं। इसमें किसी भी कानूनी या नाजायज शिशु को भी शामिल किया गया है, जिसे या तो उसके माता-पिता ने त्याग दिया है या जिसका पितृत्व प्रलेखित (डॉक्यूमेंटेड) नहीं है और एक हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख के रूप में उसे पाला गया है।
हिंदू व्यक्तिगत कानून में निर्धारित वैध दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं
- दत्तक ग्रहण करने वाला व्यक्ति दत्तक ग्रहण करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है
- दत्तक ग्रहण तब पूरा होता है जब वास्तविक रूप से देना और लेना पूर्ण हो जाता है और जब एक प्रथा जिसका नाम दाताहोमन (अग्नि आहुति) है, को किया जाता है। हालाँकि, दत्तक ग्रहण की वैधता के संबंध में यह प्रथा आवश्यक नहीं हो सकती है। बच्चे को गोद लिया जा सकता है:
- जब तक वह हिंदू है;
- उसे पहले से ही अपनाया नहीं गया है;
- जब तक भागीदारों के लिए प्रासंगिक परंपरा या प्रथा नहीं है, जो विवाहित व्यक्तियों को दत्तक ग्रहण करने की अनुमति देती है, तब तक उसकी सगाई नहीं हुई है;
- उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है जब तक कि पक्षों पर लागू होने वाली कोई प्रथा लागू नहीं होती है, जो उन्हें दत्तक ग्रहण करने में सक्षम बनाती है;
6 मार्च को एक फैसला, श्री वनाजा द्वारा दायर एक अपील के आलोक में दिया गया था, जिन्होंने स्वर्गीय नरसिम्हुलु नायडू की दत्तक बेटी को लेने का दावा किया था। उसने संपत्ति के बंटवारे के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने बाद में बर्खास्तगी की पुष्टि की। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। न्यायमूर्ति राव, जिन्होंने निर्णय लिखा था, ने 1956 के अधिनियम की धारा 7 और 11 का विरोध किया, जो दत्तक ग्रहण करने के लिए दो आवश्यक शर्तें निर्धारित करता है “1) हिंदू पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण करने से पहले पत्नी की सहमति और 2) समारोह का सबूत, वास्तविक देने और प्राप्त करने की जरूरतों को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना चाहिए।” हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार विवाह और दत्तक ग्रहण करने की उपर्युक्त प्रथाओं को पूरा करने के लिए ऊपर बताई गई शर्तों को संबंधित समुदाय की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जिसके बिना हिंदू विवाह नहीं किया जा सकता है और न ही दत्तक ग्रहण किया जा सकता है।
संवैधानिक कानून के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथाएं
संविधान “अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता (मोरेलिटी) और स्वास्थ्य के अधीन धर्म का स्वतंत्र रूप से अभ्यास, मानने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।” ‘व्यक्ति’ शब्द का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता में निहित करने के लिए निर्माताओं के सचेत (कॉन्शियस) प्रयास को दर्शाता है, चाहे वे देश के नागरिक हों या नहीं। इसके अलावा, इन अधिकारों में से प्रत्येक में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के प्रावधानों ने उस संतुलन को मूर्त रूप दिया है, जिसे संविधान ने धार्मिक अधिकारों और विकास के लक्ष्यों के बीच आकर्षित करने की मांग की थी। हालांकि, हर धर्म में अनगिनत विश्वासों को देखते हुए, सभी विश्वासों पर कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें वे भी शामिल हैं जो उस धर्म से बहुत कम संबंधित होते है या जुड़े होते है, तो अदालतों में लगभग हर दूसरे दिन प्रत्येक समुदाय द्वारा धार्मिक दावों की भरमार होती। इसलिए, अनुच्छेद 25-28 के तहत केवल धर्म की ऐसी प्रथाओं को संरक्षण दिया गया था, जो आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के अंतर्गत आती हैं।
आज तक, अदालतों ने अपने ऊपर, प्रश्न में अभ्यास की प्रकृति की पहचान करने का दायित्व ले लिया है। नतीजतन, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि “यह न्यायालय के लिए है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई प्रथा धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है या नहीं”। जब इस तरह के प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने आते हैं, तो यह उस विशिष्ट धर्म के सिद्धांतों के आलोक में उनका विश्लेषण करता है। निम्नलिखित प्रमुख परीक्षण हैं जो हालांकि सीधे न्यायालयों द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन अभ्यास की अनिवार्यता को समझते हुए उन पर विचार किया गया है।
शास्त्रों का परीक्षण
शास्त्रों को पवित्र या ईश्वर से संबंधित पाठ के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें एक विशेष धर्म पर साहित्य शामिल होता है। ज्यादातर धर्मों के अपने ग्रंथ होते हैं जो न केवल व्यक्तियों के समूह के बीच एक धार्मिक पहचान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं बल्कि प्राथमिक मान्यताओं को भी निर्धारित करते हैं जो एक विशिष्ट धर्म के अनुयायियों (फॉलोअर) का मार्गदर्शन करते हैं। धर्म और कानून दोनों के प्रति निष्पक्षता और सम्मान के प्रतीक के रूप में, अदालतें अक्सर एक अभ्यास की अनिवार्यता का आकलन करते हुए धार्मिक सिद्धांतों और साहित्य के बारे में परीक्षण करती हैं। इसलिए, धर्म ग्रंथों के साक्ष्य के माध्यम से धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन आवश्यक प्रथाओं की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नतीजतन, ऐसे मामलों को सबूतों के आधार पर या न्याय की अदालत के सामने फैसला करना अदालतों के बीच एक आम बात हो गई है।
इस प्रश्न को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक तीन तलाक के फैसले में माननीय श्री न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ का रुख था जिसने पुष्टि की और स्पष्ट किया कि धर्म से संबंधित मामलों में, ‘धर्म के रखवाले’ होने का दावा करने वालों के ज्ञान पर एकमात्र निर्भरता पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, यह एक संवैधानिक आवश्यकता है कि सावधानीपूर्वक जांच के बाद इन मान्यताओं पर भरोसा किया जाए, न कि केवल समुदाय के दावों पर। इसलिए, महत्वपूर्ण कारकों में से एक जिस पर विचार किया जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि कौन सी प्रथाएं आवश्यक हैं, वह यह है की धार्मिक ग्रंथों और सिद्धांतों में इसका स्पष्ट या निहित उल्लेख है या नहीं।
धर्म में मूल परिवर्तन का परीक्षण
प्रत्येक धर्म में एक निश्चित “विश्वासों और सिद्धांतों का एक समूह होता है, जो उन लोगों द्वारा माना जाता है जो धर्म को उनकी आध्यात्मिक भलाई के लिए अनुकूल मानते हैं।” इनमें से कुछ सिद्धांत और मान्यताएं ऐसे धर्म के दृष्टिकोण से अपरिहार्य (इनडिस्पेंसिबल) बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इसलिए, अनिवार्यता केवल उन तत्वों में से एक है जिसे यह तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या धर्म के दृष्टिकोण से एक धार्मिक प्रथा आवश्यक है या नहीं। इसलिए, धर्म के चरित्र पर इन प्रथाओं में से प्रत्येक के प्रभाव को समझकर महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रकार, यदि इस तरह की प्रथा को हटाने से धर्म की प्रकृति पर सीधे प्रभाव पड़ता है, तो इसे धर्म का अभिन्न या अनिवार्य हिस्सा माना जाएगा।
विश्वासों की सच्चाई का परीक्षण
विभिन्न अवसरों पर, अदालतों ने धार्मिक प्रथाओं के महत्व का आकलन करने पर भी जोर दिया है, जो अनुयायी (फॉलोवर्स) एक विशेष धार्मिक प्रथा से जुड़े हैं। जैसा कि न्यायमूर्ति मुखर्जी ने कहा, “मुख्य प्रश्न यह जांचने में नहीं है कि क्या कोई विशेष धार्मिक विश्वास या प्रथा हमारे औचित्य (रीजन) या भावना के अनुकूल है, लेकिन यह जांचने में है की क्या दावा किया गया विश्वास ‘वास्तव में’ और ‘ईमानदारी से’ किसी विशेष धर्म के पेशे या अभ्यास का हिस्सा माना जाता है।” यदि दावा किए गए विश्वास का पता लगाया जा सकता है कि धर्म के अनुयायियों द्वारा इसका प्रचार ईमानदारी से और वास्तव में किया गया है, तो इस प्रथा को धर्म के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में योग्य कहा जा सकता है। इसलिए, इन दावा किए गए विश्वासों की वास्तविकता का आकलन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रथाओं को अपने धर्म के लिए अभिन्न और आवश्यक माना है। इसलिए, ऐसे विश्वासों की अनिवार्यता और समग्रता (इंटीग्रालिटी) का निर्णय करते समय वास्तविकता के परीक्षण पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।
अभ्यास की प्रकृति का परीक्षण
अभ्यास की अनिवार्यता को निर्धारित करते समय, अभ्यास की प्रकृति का आकलन करना भी अनिवार्य है ताकि अभ्यास की प्रकृति के बारे मे पता लगाया जा सके और इसे अनिवार्य या वैकल्पिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए, आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत और अन्य बनाम पुलिस आयुक्त के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि तांडव नृत्य का प्रदर्शन याचिकाकर्ताओं के धर्म का एक अभिन्न या अनिवार्य हिस्सा नहीं था क्योंकि उनका धर्म सार्वजनिक रूप से ‘तांडव नृत्य’ के प्रदर्शन को अनिवार्य नहीं करता था।
तर्क के सूत्र का विस्तार करते हुए, कभी-कभी पूजा स्थल की प्रतिष्ठा और उस विशेष धर्म में इसकी भूमिका पर भरोसा किया जाता है। ऐसे पूजा स्थलों को ऊँचे स्थान पर रखा जाता है और उनके साथ “अलग और अधिक श्रद्धापूर्वक” व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद को इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं घोषित किया क्योंकि नमाज कहीं से भी पढ़ी जा सकती है।
बाधाएं और चुनौतियां: न्यायपालिका की दुविधा
धर्म के व्यापक क्षेत्र को देखते हुए, धार्मिक विश्वासों को आवश्यक या न आवश्यक में वर्गीकृत करने का कार्य हमेशा उतना सरल नहीं रहा जितना लगता है। ये विश्वास न केवल उन समुदायों का मूल हैं जो उनका पालन करते हैं, बल्कि उनके धर्म के एक महत्वपूर्ण पहलू का भी प्रतीक हैं जो पीढ़ियों से एक अभिन्न अंग रहा है। इस प्रकार, इस तरह के मामलों को संभालने के दौरान अदालतों के सामने आने वाले कठिन कार्य में, ऐसे विश्वासों की पहचान शामिल है जो पूरी तरह से अलग समय अवधि में अस्तित्व में लाए गए थे और आज के समाज की व्यावहारिक जरूरतों के अनुसार उनकी जरूरत को मापना है। जबकि ऐसा लगता है कि अदालत ने उपरोक्त परीक्षणों को तैयार करके एक विस्तृत काम किया है, साथ साथ यहां यह भी समझने की जरूरत है कि परीक्षणों का अंधाधुंध उपयोग हमेशा हमें उन मुद्दों का आदर्श समाधान प्रदान नहीं कर सकता है जो नियत समय में उत्पन्न होते हैं।
अदालत द्वारा स्थापित सिद्धांतों का एक कड़ा प्रयोग धर्म की कुछ प्राथमिक विशेषताओं की अवहेलना कर सकता है जो एक समुदाय के लोगों को एक साथ बांधते हैं। उदाहरण के लिए, केवल धर्म ग्रंथों के आधार पर धार्मिक प्रथाओं के निस्पंदन (फिल्टरेशन) को सीमित करना वास्तव में अनुयायियों की मौखिक परंपराओं का उल्लंघन हो सकता है। मौखिक परंपराएं, हालांकि लिखित नहीं हैं, ऐतिहासिक चेतना के एक सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) रूप के तरीके में स्वीकार की गई हैं जो मानव संस्कृति का एक अमूर्त हिस्सा भी बनाती हैं। वे कौशल (स्किल) या ज्ञान के रूप में मौजूद हो सकते हैं।
आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के दायरे को सीमित करना हमेशा धार्मिक विवेक के लिए खतरा माना गया है। उदाहरण के लिए, कनाडा के एक फैसले पर भरोसा करके, श्री शिरूर मैट के अनुयायियों ने मामले में अपने विश्वासों और प्रथाओं की रक्षा करने की अपनी खोज में यह भी तर्क दिया था कि “यह न्यायालय के लिए नहीं था कि वह दृढ़ विश्वास की जांच शुरू करे और इसकी वैधता का न्याय केवल कुछ उद्देश्य मानक के आधार पर करे, जैसे कि स्रोत सामग्री जिस पर दावेदार अपने विश्वास या धर्म के रूढ़िवादी (ऑर्थोडॉक्स) शिक्षण को प्रश्न में पाता है।” जैसा कि एस.पी. मित्तल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में स्वीकार किया गया है,”जो कुछ के लिए धर्म है वह दूसरों के लिए शुद्ध हठधर्मिता (डोगमा) है और जो दूसरों के लिए धर्म है वह कुछ लोगों के लिए शुद्ध अंधविश्वास है।” सबरीमाला मामले में भी इसी तरह के तर्क का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें अनुयायियों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं के विश्वासों को उन लोगों के सामने तार्किक या समझने योग्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो उन्हें साझा नहीं करते हैं।
भविष्य में क्या किया जा सकता है
यह सच है कि धर्म से संबंधित प्रथाओं या परंपराओं को खत्म करते हुए अदालतें अक्सर मुद्दों की एक श्रृंखला से घिर जाती हैं। सबसे पहले, तथ्य यह है कि उन प्रथाओं या सिद्धांतों को कानून में अपरिवर्तनीय रूप से चिपका दिया गया है, जिससे कानून की पूरी योजना को परेशान किए बिना एक हिस्से को रद्द करना असंभव हो जाता है। केवल कुछ विशेषताओं को मान्य करने और कुछ अन्य विशेषताओं को समाप्त करने से पूरे धर्म के कामकाज में बाधा आ सकती है। दूसरा, इस तरह की प्रथाएं धर्म में गहराई से निहित हैं और उस धर्म के अनुयायी अदालतों द्वारा उनकी प्रथाओं को रद्द करने से व्यथित महसूस कर सकते हैं जिससे समाज में उथल-पुथल हो सकती है।
धर्म और कानून के बीच बढ़ती हुई बातचीत आज देश के उन प्रमुख संघर्षों में से एक बन गई है जो अक्सर खुद को अदालतों का दरवाजा खटखटाता हुआ पाता है। कानून और धर्म की दो विपरीत गांठों को एक साथ जोड़ने वाली मानव डोरी को कई मौकों पर दोनों के बीच संतुलन बनाने के प्रयास में नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था उसे प्राप्त करने और अराजकता (क्योस) की स्थिति से बचने के लिए, न्यायालयों को कानून और धर्म के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए, जो समय की आवश्यकता के रूप में उभरता है वह यह है की कानून और धर्म को एक-दूसरे के साथ रखना है न कि एक-दूसरे के खिलाफ।
संदर्भ
- “The Commissioner, Hindu Religious Endowments, Madras v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar of Shri Shirur Mutt, (1954) SCR 1005 (India)”, ¶ 20
- Hindu Marriage Act 1955, s 5.
- Kamesh, ‘Conditions for A Valid, Void and Voidable Hindu Marriage’ (legalservicesindia) < http://www.legalserviceindia.com/legal/article-1487-conditions-for-a-valid-void-and-viodable-hindu-marriage.html> accessed 27 February 2021”
- Legal Correspondent, “Hindu adoption not valid without consent from wife”, The Hindu (New Delhi, March 10 2020)
- Romit Agarwal, “Adoption: Under Hindu, Muslim, Christian And Parsi Laws – Requirements for a valid adoption” (legalservicesindia) “< http://www.legalserviceindia.com/articles/hmcp_adopt.htm>” accessed on 3rdMarch 2021
- Valentina Rita Scotti, The “Essential Practice of Religion” Doctrine in India and its application in Pakistan and Malaysia, Statochiese(Feb. 8, 2016), http://203/6783-Articolo-20292-1-10-20160208.pdf(last visited July 10, 2020).
- Rahul Unnikrishnan, The Supreme Court’s tryst with religious practices (Nov. 10, 2018) https://www.barandbench.com/columns/supreme-court-tryst-religious-practices(last visited March 29, 2021)
- Durgah Committee v. Syed Hussain Ali, AIR 1961 SC 1402 (India) [hereinafter Durgah Committee]; Sankarlinga Nadan v. Raja Rajeswara Dorai, (1908) 10 (Bom. L.R.) 781 (India).
- Del Henige, Oral, but oral what? The nomenclatures of orality and their implications, Oral Tradition, 34 -47 (1988).
- David Wilson, A study on Oral Tradition as a Communication Tool, 5 Int’l J. of res. In Economics and Soc.Sci.,118-124(2014) ; Zee Entertainment Enterprises v. Mr. Gajendra Singh, 2008 36 PTC 53 Bom. (India).



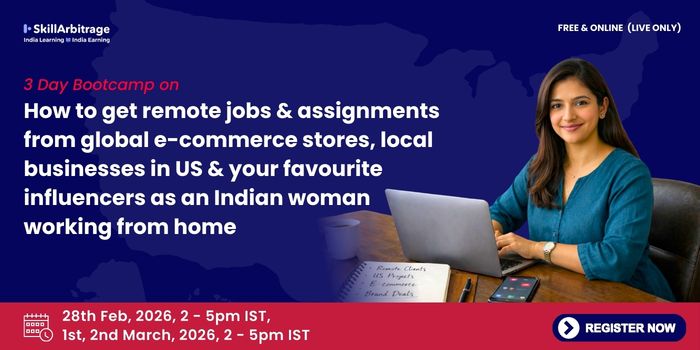





Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. Its always helpful to read through articles from other writers and use something from their web sites.