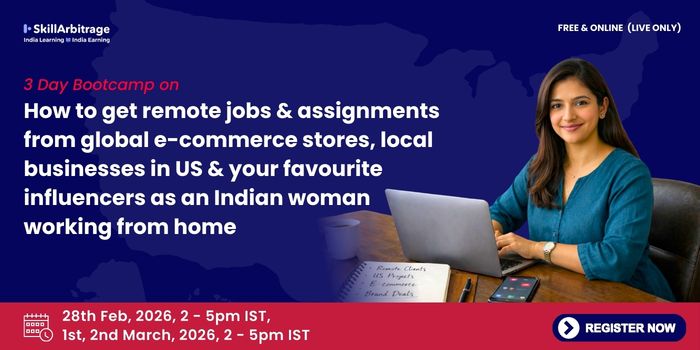यह लेख गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, पंजाब की Nidhi Bajaj द्वारा लिखा गया है। लेख आपको क़ानूनों की व्याख्या के महत्वपूर्ण सिद्धांत/कहावत अर्थात्, ‘अट रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेट’ के अर्थ, आधार और अनुप्रयोग के बारे में बताएगा। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
“जब तक शब्द इतने अर्थहीन नहीं थे कि मैं उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे कुछ अर्थ खोजने के लिए बाध्य होना चाहिए, और उन्हें अनिश्चितता के लिए शून्य घोषित नहीं करना चाहिए” – फारवेल जे।
कहावत ‘यट रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेट:’ कानूनों की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका शाब्दिक अर्थ है: “यह शून्य के बजाय क्रियाशील हो सकता है”। इस कहावत का प्रभाव यह है कि एक अधिनियमित प्रावधान या एक क़ानून को प्रभावी और क्रियाशील बनाने के लिए इस तरह से माना जाना चाहिए।
बिना किसी देरी के, आइए हम इस कानूनी कहावत के अर्थ और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने का प्रयास करते है।
अट रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरीट का अर्थ
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कहावत ‘अट रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेट’ का अर्थ है कि किसी चीज़ के लिए शून्य होने की तुलना में प्रभाव होना बेहतर है। किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय, अदालतों को ऐसे अर्थ करना की ओर नहीं झुकना चाहिए जो किसी भी प्रावधान या क़ानून को शून्य या व्यर्थ बनाता है। इसलिए, जब भी किसी प्रावधान में उपयोग किए जाने वाले शब्द गलत, अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं, जिससे वैकल्पिक अर्थ करना की संभावना होती है, तो अदालतों को प्रावधान को इस तरह से समझना चाहिए कि क़ानून का कोई भी प्रावधान निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) न हो।

अटी रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेट का आधार
कहावत अट रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेट निम्नलिखित सिद्धांतों और अनुमानों पर आधारित है:
- किसी क़ानून को सरासर अस्पष्टता के लिए शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- जब अदालतें किसी प्रावधान की व्याख्या शुरू करती हैं, तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि कानून जीवित रहे।
- किसी क़ानून की संवैधानिकता पर फैसला सुनाते समय, अदालतों को इसकी संवैधानिकता के पक्ष में अनुमान से शुरू करना चाहिए।
- किसी प्रावधान या क़ानून की सही व्याख्या वह है जो विधायिका के इरादे के अनुसार है। विधायिका का इरादा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क़ानून के सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाने के अलावा अन्यथा नहीं हो सकता है जिसके लिए कानून बनाया गया था।
- ऐसी व्याख्या अपनाना जिसके द्वारा किसी भी प्रावधान को निष्क्रिय या अव्यावहारिक बना दिया जाता है, विधायी इरादे के प्रतिकूल होगा।
- अदालतों को कानून की व्याख्या करनी है और कानून बनाना और निरस्त करना विधायिका का अनन्य अधिकार क्षेत्र है। ऐसी परिस्थितियों में, कोई भी व्याख्या जिसके द्वारा कोई भी प्रावधान या क़ानून व्यर्थ हो जाता है, कानून की अस्वीकृति के बराबर है और यह अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
- अदालतें असंवैधानिकता के आधार पर किसी कानून को रद्द कर सकती हैं, लेकिन अदालतें एक अजीबोगरीब अर्थ करना को अपनाकर या किसी विशेष तरीके से किसी प्रावधान का अर्थ करना करके किसी प्रावधान में कोई अस्पष्टता या असंवैधानिकता पेश नहीं कर सकती हैं।
भारतीय मामलों में इस कहावत को लागू करना
अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1965) न्यायालय
इस मामले में, विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 39 की व्याख्या के संबंध में प्रश्न उठा। अपीलकर्ता को विद्युतअधिनियम की धारा 39 के तहत पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की चोरी के लिए दोषी ठहराया गया था और प्रतिवादी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 379 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील में, उन्होंने इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी कि उन्होंने चोरी की थी, लेकिन केवल कानून का सवाल उठाया कि कुछ वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर उनकी दोषसिद्धि अवैध थी।
भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 39 में प्रावधान किया गया था कि, “जो कोई भी बेईमानी से सार तत्वों का उपयोग करता है, किसी भी ऊर्जा का उपभोग करता है या उपयोग करता है, उसे भारतीय दंड संहिता के अर्थ के भीतर चोरी करने वाला माना जाएगा”। इसलिए, धारा 39 के अनुसार, दोषी पाए गए अभियुक्त को आईपीसी की धारा 379 के तहत दंडित किया जाएगा।
भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 50 निम्नलिखित शर्तों में दोषसिद्धि की प्रक्रिया प्रदान करती है: अधिनियम के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जाएगा…। सरकार या विद्युत निरीक्षक या उससे पीड़ित व्यक्ति के कहने को छोड़कर।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे धारा 39 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि धारा 50 के तहत दोषसिद्धि की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अपीलकर्ता के अनुसार, उसका अभियोजन खराब और अक्षम था क्योंकि यह सरकार या एक विद्युत निरीक्षक या चोरी से पीड़ित व्यक्ति के इशारे पर नहीं था।
न्यायालय ने कहा कि चूंकि अपराध विद्युत अधिनियम के खिलाफ है, न कि आईपीसी के खिलाफ, इसलिए धारा 50 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया।
इस प्रकार, इस मामले में, न्यायालय ने धारा 50 को निष्क्रिय और व्यर्थ बनाने वाले अर्थ करना से बचने के लिए अधिकतम सीमा लागू की।
केबी नागपुर, एमडी (आयुर्वेदिक) बनाम भारत संघ (2012) सर्वोच्च न्यायालय
इस मामले में, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 7 (1) के अर्थ करना के संबंध में सवाल उठा। उक्त प्रावधान में कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या केंद्रीय परिषद के सदस्य तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी को विधिवत निर्वाचित या नामित नहीं किया जाएगा। खंड “या जब तक उनके उत्तराधिकारी को विधिवत निर्वाचित या नामित (ड्यूली एलेक्टेड और नॉमिनेटेड) नहीं किया जाएगा, जो भी अधिक हो” को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई थी।
सर्वोच्च नियालयने धारा 7 (1) की संवैधानिकता को बरकरार रखा और कहा कि उक्त प्रावधान संसद द्वारा उन स्थितियों का ध्यान रखने के लिए किया गया था जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सदस्य के पद के चुनाव में विभिन्न कारणों से देरी होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि केंद्रीय परिषद की सदस्यता में कोई खालीपन न हो। इस प्रकार न्यायालय ने धारा 7 (1) का अर्थ लगाया ताकि इसे प्रभावी और क्रियाशील बनाया जा सके।
डी. सलबाबा बनाम भारत की विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) (2003) सर्वोच्च न्यायालय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 48AA की व्याख्या का सवाल आया था। याचिकाकर्ता, एक शारीरिक रूप से विकलांग वकील, विकलांग व्यक्ति के कोटे में आवंटित एक एसटीडी बूथ भी चला रहा था। पेशेवर कदाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी। दिनांक 20-2-2001 को भारत की विधिज्ञ परिषद ने उन्हें बूथ वापस करने का निर्देश दिया लेकिन वह विनिदष्ट समयावधि में ऐसा करने में विफल रहे। भारत की विधिज्ञ परिषद ने दिनांक 31-3-2001 को एक आदेश दिया जिसमें राज्य बार काउंसिल को अधिवक्ताओं की सूची से अधिवक्ता का नाम हटाने का निर्देश दिया गया। अधिवक्ता ने बाद में बूथ को आत्मसमर्पण कर दिया और बार काउंसिल के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की। उनकी याचिका 26-8-2001 को इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि यह सीमा द्वारा निषिद्ध है। वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।
अधिवक्ता अधिनियम की धारा 48AA उस आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारत की विधिज्ञ परिषद के निर्णय/आदेश की समीक्षा का प्रावधान करती है। धारा 48AA का अर्थ लगाते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘उस आदेश की तारीख से साठ दिन’ शब्द को पढ़ा जाना चाहिए ताकि आदेश के संचार, ज्ञान, वास्तविक या रचनात्मक की तारीख की समीक्षा की जाए। इस नियम को लागू करते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार धारा 48AA की व्याख्या की ताकि इसे वास्तव में प्रभावी बनाया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की विधिज्ञ परिषद के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता का नामांकन बहाल कर दिया गया।
कलकत्ता विश्वविद्यालय और अन्य बनाम प्रीतम रूज (2009) कलकत्ता उच्च न्यायालय
इस मामले में, एक छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण की मांग करते हुए एक आरटीआई आवेदन किया, जिसे पीआईओ यानी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) के तहत छूट का दावा करते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद, आवेदक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें एक विशेषज्ञ परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को पेश करने की मांग की गई। न्यायालय के समक्ष दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण आए, एक सार्वजनिक प्राधिकारियों का विचार था कि आरटीआई अधिनियम की प्रयोज्यता और संचालन प्रणाली को अव्यवहारिक बना देगा और दूसरा सूचना चाहने वालों को इसके द्वारा प्रदत्त अधिकार के कारण उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।
अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, अटी रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेट के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और सीबीएसई को सूचना चाहने वालों को उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण देने का निर्देश दिया, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के बारे में याचिका को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे छात्रों के लिए उचित कार्यवाही में इस ओर से राहत मांगने का विकल्प खुला रह गया। न्यायालय नोक्स बनाम डोनकास्टर अमलगमेटेड कोलियरीज लिमिटेड (1940) के फैसले से सहमत था, जिसमें यह माना गया था कि जहां विकल्प दो व्याख्याओं के बीच है, जिनमें से संकीर्णता कानून के स्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होगी, एक अर्थ करना होगा जो कानून को निरर्थक बनाने से बचाएगा और इस विचार के आधार पर साहसिक (बोल्डर) अर्थ करना (कंस्ट्रक्शन) को स्वीकार किया जाना चाहिए कि संसद केवल प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय का विचार
- तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम असम राज्य (1990) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतें अर्थ करना के खिलाफ दृढ़ता से झुकती हैं जो एक क़ानून को निरर्थकता में बदल देता है। किसी कानून या उसमें किसी अधिनियमित प्रावधान का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वह प्रभावी और क्रियाशील हो सके। हालांकि, यदि कोई क़ानून पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसकी भाषा पूरी तरह से असाध्य और बिल्कुल अर्थहीन है, तो क़ानून को अस्पष्टता के लिए शून्य घोषित किया जा सकता है।
- शंकर राम एंड कंपनी बनाम काशी नायकर (2003) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक धारणा मौजूद है कि विधायी इरादा क़ानून के हर हिस्से को प्रभावी बनाना है। यह अर्थ करना का एक प्रमुख नियम है कि आम तौर पर किसी भी शब्द या प्रावधान को किसी क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करने में अनावश्यक नहीं माना जाना चाहिए। यह कहना सही नहीं है कि किसी क़ानून में एक शब्द अनावश्यक या उद्देश्यहीन है जब तक कि क़ानून की योजना और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहने के लिए बाध्यकारी कारण न हों जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।
- महाराष्ट्र भूमि विकास निगम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) मामले में, सर्वोच्च नियालय ने कहा कि एक क़ानून के प्रत्येक शब्द और वाक्यांश को उसके संदर्भ में समझा जाना चाहिए और इसे महत्व दिया जाना चाहिए ताकि यह निरर्थक न हो जाए।
- बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे (2014) मामले में, सर्वोच्च नियालय ने माना कि जहां वैकल्पिक अर्थ करना की संभावना है, वहां अदालत को ऐसे अर्थ करना को अपनाना चाहिए जो उस प्रणाली के सुचारू कामकाज को सक्षम करे जिसके लिए क़ानून लागू किया गया है और अर्थ करना जो क़ानून के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा बन जाता है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। एक अर्थ करना जो कानून को निरर्थक बना देता है, उससे बचा जाना चाहिए।
- स्वामी आत्मानंद बनाम श्री रामकृष्ण तपोवनम (2005) मामले में, सर्वोच्च नियालय द्वारा यह माना गया था कि क़ानून को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। एक क़ानून को यथोचित रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसे व्यावहारिक बनाने के तरीके से समझा जाना चाहिए।
- एच.एस. वांकानी बनाम गुजरात राज्य (2010) मामले में सर्वोच्च नियालय ने कहा कि मैक्सिम यू रेस मैगिस वैलेट क्वाम पेरेट का यह भी अर्थ है कि जहां क़ानून का स्पष्ट इरादा इसे लागू करने में बाधाओं को जन्म देता है, तो अदालत को बेतुके परिणामों से बचने के लिए उन बाधाओं को दूर करने के तरीके खोजने चाहिए। यह कानूनों की व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि अर्थ करना को एक वैधानिक प्रावधान पर नहीं रखा जाना चाहिए जो प्रकट बेतुकापन, निरर्थकता, स्पष्ट अन्याय और बेतुकी असुविधा या विसंगति को जन्म दे।

निष्कर्ष
फॉसेट प्रॉपर्टीज बनाम बकिंघम काउंटी काउंसिल के मामले में लॉर्ड डेनिंग ने कहा है कि “जब किसी क़ानून का कुछ अर्थ होता है, भले ही वह अस्पष्ट हो, या कई अर्थ हों, भले ही उनके बीच चुनने के लिए बहुत कम हो, अदालतों को यह कहना होगा कि क़ानून का क्या अर्थ है, बजाय इसे शून्य के रूप में अस्वीकार करने के।
विधायिका किसी प्रावधान या क़ानून में अनावश्यक या महत्वहीन शब्दों का उपयोग नहीं करती है, और इसलिए, क़ानून में किसी भी शब्द या शर्तों की व्याख्या करते समय एक अर्थ करना जो क़ानून को क्रियाशील बनाता है और शब्दों को प्रासंगिक बनाता है, उसे उस व्यक्ति के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो शब्दों को अप्रभावी, शून्य और बेकार बनाता है।
संदर्भ
- D.N. Mathur, Interpretation of Statutes, Fifth Edn.
- GP Singh: Principles of Statutory Interpretation, 14th Edn.
- Prof. T. Bhattacharya, The Interpretation of Statutes