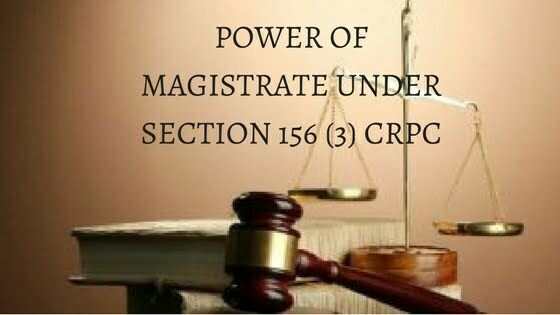यह लेख सिंबायोसिस लॉ स्कूल, नागपुर के छात्र Arryan Mohanty द्वारा लिखा गया है। यह लेख आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 के प्रावधानों के बारे में बात करता है, जो संज्ञेय (कॉग्निजेबल) मामलों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है। लेख में विशेष रूप से धारा 156(3) और उससे संबंधित न्यायिक घोषणाओं पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रक्रिया को तीन चरणों: जांच, पूछताछ और विचारण (ट्रायल) में विभाजित किया गया है। भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत हर अपराध का जांच, पूछताछ और विचारण आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में उल्लिखित चरणों के तहत किया जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 2(h) के अनुसार, “जांच” इस संहिता द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की गई सभी कानूनी कार्रवाइयों को संदर्भित करता है, चाहे एक पुलिस अधिकारी, एक मजिस्ट्रेट के अलावा कोई व्यक्ति, या दोनों उन्हें करते हों।
जांच एक जटिल या गुप्त चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक व्यवस्थित, सावधानीपूर्वक और गहन प्रयास है; यह अक्सर औपचारिक (फॉर्मल) और आधिकारिक होता है। यह सूचना एकत्र करने, वस्तुओं को स्थानांतरित (मूव) करने और प्रासंगिक जानकारी की तलाश करने को संदर्भित करता है। पुलिस जांच करती है, जो प्रारंभिक चरण है, और वे आम तौर पर प्राथमिकी (एफआईआर) दाखिल करने के बाद जांच शुरू करते हैं। हालांकि वाक्यांश “प्राथमिकी” का स्पष्ट रूप से सीआरपीसी में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आम तौर पर इसका मतलब यही होता है।
कोई भी पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना देकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के बाद पुलिस को जांच शुरू करने और मामला दर्ज करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है।
संहिता की धारा 154(1) के अनुसार, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी गई संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई भी जानकारी, मौखिक रूप में या लिखित रूप में होनी चाहिए और अगर इसे मौखिक रूप में दिया गया है तो इसे लिखित में करना चाहिए और मुखबिर द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। उक्त जानकारी को प्राथमिकी में शामिल किया जाना चाहिए जब इसे लिखित रूप में किया गया हो।
हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्राथमिकी एक आवश्यक दस्तावेज है। मुखबिर के दृष्टिकोण से, इसका प्राथमिक लक्ष्य आपराधिक न्याय प्रणाली को चालू करना है। जांच अधिकारियों के दृष्टिकोण से, यह कथित अवैध गतिविधि के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है ताकि दोषियों को खोजने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।
कई लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है, जहां पुलिस अधिकारियों को शिकायत सुननी चाहिए या दर्ज करनी चाहिए। पुलिस अधिकारी, हालांकि, शिकायत या प्राथमिकी दर्ज करने से रोकता है क्योंकि एक बार दर्ज होने के बाद, पुलिस अधिकारी को कार्रवाई करनी चाहिए या स्थिति को देखना चाहिए।
नतीजतन, पुलिस अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का फैसला किया। सर्वोच्च न्यायालय ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश की सरकार और अन्य में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शिकायत मिलने पर अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए; इस दायित्व को पूरा करने के लिए पुलिस अधिकारी की आवश्यकता है।
सीआरपीसी की धारा 156(3) के कारण ऐसे पीड़ितों के पास अब पुलिस द्वारा मामले की जांच कराने का विकल्प है। मजिस्ट्रेट को शिकायत की जा सकती है, जो तब पुलिस को जांच करने का आदेश दे सकता है। इस बार, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की अवहेलना या इनकार नहीं कर सकती है, जिससे जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मजिस्ट्रेट केवल एक साधारण कार्यालय नहीं है। उसे विश्वास होना चाहिए कि पुलिस द्वारा जांच करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) है। हालांकि, आपराधिक कानून के कुछ मूलभूत सिद्धांत, जैसे शिकायत, जांच, पूछताछ, संज्ञान (कॉग्निजेंस) आदि, ऐसी संतुष्टि की अवधारणा और संतुष्टि के आधार की सराहना करने के लिए समझ में आने चाहिए।
सीआरपीसी की धारा 156 किस बारे में बात करती है
सीआरपीसी की धारा 156 के अनुसार, पुलिस को औपचारिक प्राथमिकी या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक अपराध की जांच करने की अनुमति है। यदि पुलिस जांच नहीं करती है तो मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दे सकता है। हालांकि, मजिस्ट्रेट ऐसा करने पर पुलिस को जांच करने से नहीं रोक सकते है।
न्यायालयों को जांच करने के पुलिस के वैधानिक अधिकार को प्रतिबंधित करने या हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया गया है। जब पुलिस जांच के बाद आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल करती है तो अदालतें कार्रवाई कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन उनकी भूमिका वहीं से शुरू हो जाती है।
मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी अपराध की जांच करने के लिए पुलिस को धारा 156(1) के तहत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। न्यायपालिका पुलिस के कानूनी जांच अधिकारों में हस्तक्षेप या नियमन नहीं कर सकती है। पुलिस को जांच करने की अनुमति नहीं है अगर प्राथमिकी या अन्य प्रासंगिक दस्तावेज किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की जानकारी देने में विफल होते हैं।
ऐसी स्थिति में, उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जांच को रोक सकता है और रद्द कर सकता है। पुलिस धारा 156(1) के तहत अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन) के बाहर संज्ञेय अपराधों की जांच कर सकती है। मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2016) के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार मामले में, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संहिता का अध्याय XIII “पूछताछ और विचारण में आपराधिक अदालतों के क्षेत्राधिकार” को स्थापित करता है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्याय, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, में कई प्रावधान शामिल हैं जो अदालत को एक आपराधिक मामले की जांच करने या मुकदमा चलाने का अधिकार देते हैं और किसी दिए गए क्षेत्र के बाहर किए गए अपराधों की जांच, पूछताछ या विचारण पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
धारा 177 से 188 के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाएगा। संहिता की धारा 177 और 178 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि धारा 177 एक जांच या विचारण के लिए एक “साधारण” स्थान स्थापित करती है।
जब यह स्पष्ट नहीं है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया था, या अपराध कहाँ किया गया था, जब अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया गया था, या जब इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल थे, धारा 178 जांच या विचारण के लिए एक स्थान प्रदान करती है। इनमें से किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा इसकी जांच या विचारण किया जा सकता है।
इसलिए, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि अपराध की जांच के लिए एसएचओ को अधिक क्षेत्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता है। हालांकि, अगर अधिकारी जांच के बाद यह निर्धारित करता है कि प्राथमिकी दर्ज करने का कारण उसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो वह मामले को संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत (ऑथराइज्ड) है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा अधिकारी जांच को मुकदमे की ओर ले जाता है, मामले का परिणाम-दोषसिद्धि या दोषमुक्ति-अप्रभावित रहता है।
यह मुख्य रूप से विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। अपराध की कोई भी अनुचित या अधूरी जांच विचारण को अमान्य नहीं करती है जब तक कि यह अभियुक्त के खिलाफ पूर्वाग्रह या न्याय के उल्लंघन का कारण न बने।
हरि सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) में यह निर्णय लिया गया कि यदि पुलिस घटना की जाँच करने में विफल रही तो शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत ला सकता है। हालांकि, शिकायतकर्ता की रिट याचिका में सीबीआई से जांच करने के लिए कहना अनुचित है।
जांच का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्तियां
सीआरपीसी की धारा 190 के तहत संज्ञान लेने के लिए अधिकृत एक मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 156(3) के तहत किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने का अधिकार दिया जाता है, जो पूर्व-संज्ञेय स्तर पर लागू होता है।
सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अनुसार धारा 190 द्वारा अधिकृत मजिस्ट्रेट एक पुलिस अधिकारी को जांच करने का निर्देश दे सकता है यदि पुलिस प्राधिकरण (अथॉरिटी) अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहता है, जो कि शिकायत या प्राथमिकी दर्ज करना है। यह खंड तब लागू होता है जब कोई पुलिस अधिकारी शिकायत या प्राथमिकी दर्ज करता है, लेकिन पूरी तरह से जांच करने में विफल रहता है। “कोई भी मजिस्ट्रेट” शब्द न्यायिक मजिस्ट्रेट को संदर्भित करता है जो एक संज्ञेय अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है न कि कार्यकारी (एग्जिक्यूटिव) मजिस्ट्रेट। कार्यकारी मजिस्ट्रेट संज्ञेय अपराध की जांच का निर्देश नहीं दे सकते है।
इस उपधारा के पास जांच करने के लिए धारा 202(1) के समान अधिकार नहीं है। धारा 156(3) और धारा 202(1) का प्रयोग क्रमशः पूर्व-संज्ञेय और पश्च-संज्ञेय चरणों में किया जाता है।
धारा 190(1)(a) के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले गंभीर अपराध होने की शिकायत की स्थिति में मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। एक मजिस्ट्रेट इस प्रावधान के तहत जांच शुरू नहीं कर सकता है।
एक बार जब पुलिस जांच के योग्य अपराध की जांच शुरू कर देती है, तो मजिस्ट्रेट जांच नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि पुलिस ने संहिता की धारा 156(3) के तहत संज्ञान लेने से पहले और पुलिस की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त करने से पहले अपने जांच के कर्तव्यों में बेईमानी से काम किया। उस मामले में, उसके पास शिकायतकर्ता को सूचित करने, उनका बयान दर्ज करने और किसी भी अतिरिक्त गवाहों के बयान दर्ज करने और संहिता की धारा 204 के तहत एक प्रक्रिया जारी करने का अधिकार है।
इस संदर्भ में निम्नलिखित शर्तें स्पष्ट हो जाती हैं:
- कानून एक मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने की अनुमति नहीं देता है जब वह अध्याय XIV के प्रावधानों के तहत नोटिस लेने का विकल्प चुनता है। इसके बजाय, वह पूर्व-संज्ञान चरण के दौरान धारा 190, 200 और 204 के तहत संज्ञान लेने से पहले ही ऐसा कर सकता है। हालांकि, वह एक पुलिस जांच का निर्देश दे सकता है – संहिता की धारा 202 द्वारा वर्णित जांच की तुलना में – ऐसी परिस्थितियों में जो इस धारा के परंतुक (प्रोविजो) के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- ऐसे मामलों में जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने का फैसला करता है, तो वह नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से चुन सकता है:
- वह शिकायत को पढ़ सकता है, और यदि वह तय करता है कि आगे बढ़ने के वैध कारण हैं, तो वह तुरंत अभियुक्त को सम्मन कर सकता है। हालाँकि, उसे पहले धारा 200 के मानदंडों (क्राइटेरिया) का पालन करना होगा और शिकायतकर्ता या उसके गवाहों की गवाही दर्ज करनी होगी।
- मजिस्ट्रेट प्रक्रियात्मक मामलों में देरी कर सकता है और स्वयं एक स्वतंत्र जाँच की निगरानी कर सकता है।
- मजिस्ट्रेट प्रक्रियात्मक विवाद को स्थगित कर सकता है और पुलिस जांच या किसी अन्य व्यक्ति को जांच करने का आदेश दे सकता है।
- यदि मजिस्ट्रेट आश्वस्त (कन्विंस्ड) नहीं है कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान की समीक्षा करने के बाद या जांच के आदेश के परिणामस्वरूप आगे बढ़ने के पर्याप्त कारण हैं, तो वह शिकायत को खारिज कर सकता है।
- जब एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत संज्ञान लेने से पहले पुलिस जांच का आदेश देता है और रिपोर्ट प्राप्त करता है; नतीजतन, उसके पास कई विकल्प होते हैं। वह रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकता है और अभियुक्त को रिहा कर सकता है, अभियुक्त के खिलाफ औपचारिक आरोप जारी कर सकता है, या उसके ध्यान में लाई गई शिकायत पर विचार कर सकता है और संहिता की धारा 190 के तहत कार्रवाई कर सकता है।
मजिस्ट्रेट धारा 156(3) की शक्ति का प्रयोग संज्ञान लेने से पहले कर सकता है। इसने पुलिस को अपने पूर्ण जांच अधिकार का उपयोग करने के लिए एक सक्रिय अनुस्मारक (रिमाइंडर) या निर्देश के रूप में कार्य किया, जो धारा 156 से शुरू होता है और धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट या आरोप पत्र (चार्जशीट) के साथ समाप्त होता है।
दूसरी ओर, धारा 202 संज्ञान के बाद के चरण के दौरान लागू होती है, और जांच को यह निर्धारित करने के लिए सौंपा गया था कि क्या जारी रखने के लिए पर्याप्त औचित्य था। नतीजतन, मजिस्ट्रेट को अपना फैसला लागू करने के बाद ही धारा 156(3) के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिए।
निर्दिष्ट खंड के अनुसार एक निर्देश जारी किया जाता है जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से इनकार करता है, किसी मामले को स्थगित करना आवश्यक नहीं समझता है, और यह निर्धारित करता है कि इसके विचारण के लिए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए।
दूसरे शब्दों में, ऐसा निर्देश तब जारी किया जाता है जब उपलब्ध सामग्री की विश्वसनीयता या न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए जांच को तुरंत निर्देशित करना स्वीकार्य माना जाता है। न्याय का हित निर्देशित करता है की मजिस्ट्रेट के निर्णय को एक मामले से दूसरे मामले में है संहिता की संरचना से तैयार किए गए इन बुनियादी सिद्धांतों के अधीन होना चाहिए।
सीबीआई और अन्य बनाम राजेश गांधी और अन्य (1996), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “कोई भी अनुरोध नहीं कर सकता है कि एक विशेष एजेंसी एक उल्लंघन की जांच करे।” इस दृष्टिकोण को साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2007) में स्वीकार किया गया था।
इस मामले में आगे यह फैसला सुनाया गया कि अगर किसी व्यक्ति की शिकायत है कि पुलिस थाने में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है, तो वह संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस अधीक्षक को लिखित में आवेदन दे सकता है।
पीड़ित पक्ष विचाराधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) के लिए आवेदन कर सकता है, भले ही उसका परिणाम संतोषजनक न हो, जिसका अर्थ है कि या तो प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई है या दर्ज होने के बाद भी कोई उचित जांच नहीं हो पाई है। इसलिए, धारा 156(3) के तहत एक मामला दर्ज करने के लिए, दो आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:
- एसपी और थाने ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
- हालांकि एसपी व थाना पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली, लेकिन पर्याप्त जांच नहीं हुई है।
एक न्यायिक अधिकारी को उन मामलों में विशेष अधिकार दिया जाता है जहां पुलिस मनमाने ढंग से प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निर्णय से पहले, पीड़ित पक्ष संहिता की धारा 482 पर प्रयोग करते थे।
चूंकि पीड़ितों को अब धारा 156(3) के तहत अदालत में जाना पड़ता था, अगर उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती थी, तो उपरोक्त निर्णय ने मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार प्रदान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर एम. सुब्रमण्यम और अन्य बनाम एस. जानकी और अन्य (2020), के मामले में साकिरी वासु के फैसले की पुष्टि सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे और अन्य (2010) में न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला देते हुए, की।
पीड़ित पक्ष के लिए उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाना नहीं है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है, अगर उन्हें शिकायत है कि पुलिस ने उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है या एक उचित जांच नहीं हो रही है।
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस की शक्तियां
धारा 156(3) की जांच के लिए मजिस्ट्रेट से आदेश केवल पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रमेश अवस्थी बनाम दिल्ली राज्य (2017) में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हाल ही के निर्णय के अनुसार, मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के बाहर एक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को कोई आदेश या शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2001) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर था, भले ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 सूचना प्राप्त करने वाले प्रभारी अधिकारी को इसे दर्ज करने से प्रतिबंधित करती है, धारा 155 और 156 प्रभारी व्यक्ति को थाने की सीमाओं के भीतर किए गए अपराधों को देखने का अधिकार देती है।
इसलिए, एक मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार है कि वह थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी को थाने में स्थानीय क्षेत्राधिकार के अधीन एक संज्ञेय अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकता है। परिणामस्वरूप एक मजिस्ट्रेट को प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को बनाए रखना चाहिए। मान लीजिए कि ऊपर वर्णित अपराध का विचारण करने की शक्ति का अभाव है। यदि हां, तो वह धारा 156(3) के तहत आदेश जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना था कि क्या एक मजिस्ट्रेट सीबीआई को धारा 156 के तहत एक अपराध की जांच करने का निर्देश दे सकता है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था। “हमें उस मुद्दे के दायरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है,” अदालत ने फैसला सुनाया, “चूंकि मौजूदा विवाद इस बात तक सीमित है कि क्या एक मजिस्ट्रेट सीबीआई को धारा 156 (3) के तहत अपने क्षेत्राधिकार के तहत जांच करने के लिए कह सकता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार सब-मजिस्ट्रेट का अधिकार एक पुलिस थाने के कार्यालय को जांच करने का निर्देश देने तक सीमित है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की पीठ ने महाराष्ट्र राज्य बनाम इब्राहिम ए पटेल (2007) के मामले में अपने फैसले में एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य व्यक्त किया। यह माना गया था कि मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 190 के तहत एक अपराध का संज्ञान लेने और धारा 156(3) की सीधी व्याख्या के आधार पर पुलिस थाने के प्रभारी किसी भी पुलिस अधिकारी को जांच करने का निर्देश देने का अधिकार है। एक अधिकारी ऐसे पुलिस थाने के आसपास के परिबद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए योग्य है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय का इस क्षेत्र पर अधिकार है।
मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत केवल अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थाने के एसएचओ (प्रभारी अधिकारी) को जांच का निर्देश दे सकता है। यह स्थापित कानूनी मिसाल के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है।
एक मजिस्ट्रेट को किसी वरिष्ठ (सुपीरियर) पुलिस अधिकारी, किसी अन्य जांच एजेंसी (जैसे सीबीआई या सीआईडी), या अपने प्रदेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को धारा 156(3) द्वारा उसे दिए गए अधिकार का उपयोग करके जांच का आदेश देने की अनुमति नहीं है। इससे पता चलता है कि मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकता है अगर मजिस्ट्रेट के प्रदेशिक क्षेत्राधिकार के बाहर किए गए अपराध का दावा किया जाता है।
सीआरपीसी की धारा 156 (3) कब लागू होती है
मोहम्मद यूसुफ बनाम श्रीमती आफाक जहां और अन्य (2006) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध की सूचना लेने से पहले संहिता की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे शिकायतकर्ता को शपथ लेने के लिए मजबूर करने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह किसी गलत काम से अनजान था।
मजिस्ट्रेट पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे सकता है ताकि वे जांच शुरू कर सकें। ऐसा करना कानून के खिलाफ नहीं है। आखिरकार, संहिता की धारा 154 में कहा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस थाने के प्रभारी व्यक्ति द्वारा रखी गई एक किताब में संज्ञेय अपराध के होने के बारे में आवश्यक विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह शिकायत द्वारा प्रकट किए गए संज्ञेय अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करे, भले ही एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 156(3) के तहत स्पष्ट रूप से जांच का निर्देश नहीं देता है कि एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि वह पुलिस अधिकारी उसके बाद ही संहिता के अध्याय XII में विचार किए गए अन्य कदम उठा सकते हैं।
इस न्यायालय ने दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007) के मामले में भी यही रुख अपनाया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अगर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस ने एक जांच की है लेकिन पीड़ित व्यक्ति संतोषजनक नहीं पाता है, तो वह व्यक्ति अभी भी संहिता की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है।
यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है, तो वे उचित जांच का आदेश दे सकते हैं और अन्य उचित कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए, यदि मजिस्ट्रेट का मानना है कि पुलिस को अपना काम सही ढंग से करने की आवश्यकता है या मामले की जांच से असंतुष्ट है, तो वह पुलिस को जांच की निगरानी करने का आदेश दे सकता है।
विनुभाई हरिभाई मालवीय और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2019), में कानूनी मुद्दा यह था कि क्या मजिस्ट्रेट के पास पुलिस द्वारा आरोप पत्र दायर करने के बाद आगे की जांच का आदेश देने का अधिकार है और यदि हां, तो आपराधिक मामले के किस चरण तक जांच की गई थी। कई मिसालों और प्रासंगिक विधायी प्रावधानों का हवाला देने के बाद, यह निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास व्यापक विवेकाधिकार है क्योंकि इस न्यायिक प्राधिकरण को संतुष्ट होना चाहिए कि पुलिस द्वारा एक वैध जांच की जाती है।
संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास प्रासंगिक या निहित शक्तियों सहित सभी आवश्यक शक्तियों तक पहुंच होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक ‘उचित जांच’ – पुलिस द्वारा एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण जांच के रूप में परिभाषित होती है, जिसे मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण करना है। इस शक्ति में निस्संदेह धारा 173(2) के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त जांच का आदेश देना शामिल है। कथात्मक रूप से भी, सीआरपीसी की धारा 156(1) में उल्लिखित “जांच” में, धारा 2(h) के तहत “जांच” की परिभाषा के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए सबूतों को इकट्ठा करने के लिए कोई भी कार्यवाही शामिल होगी; इसमें निस्संदेह संहिता की धारा 173(8) के तहत एक और जांच के माध्यम से कार्यवाही होगी।
एक मजिस्ट्रेट धारा 156 (3) के तहत पूर्व और बाद के संज्ञान चरणों में अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है यदि कोई निर्णायक कानूनी मिसाल है। शक्ति में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को मामला दर्ज करने और जांच करने के निर्देश देना शामिल हो सकता है।
एक मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उन मामलों में उचित जांच करने और औपचारिक जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है, जिसमें प्रक्रिया की निगरानी करना शामिल है, जहां प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है।
जब कोई पीड़ित या शिकायतकर्ता अनुरोध करता है कि एक मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे, तो उन्हें धारा 154(1) और 154(2) में उल्लिखित सभी चरणों का पालन करना चाहिए। अदालत ने प्रियंका श्रीवास्तव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) में कहा कि इस देश में एक चरण आ गया है जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के आवेदनों को मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आह्वान की मांग करने वाले आवेदक द्वारा विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है।
इसके अलावा, विद्वान मजिस्ट्रेट सही परिस्थितियों में तथ्यों और आरोपों की सत्यता की जांच करने में बुद्धिमान होंगे। इस हलफनामे (एफिडेविट) के लिए आवेदक अधिक जिम्मेदार बन सकता है। इसके अलावा, यह तब और भी परेशान करने वाला और डरावना हो जाता है जब कोई वैधानिक प्रावधान के तहत आदेश देने वालों को ट्रैक करने की कोशिश करता है जिसे संबंधित अधिनियम या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी जा सकती है।
हालांकि, आपराधिक अदालत में गलत तरीके से व्यवहार करना कानून के खिलाफ है, जैसे कि कोई हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा हो। धारा 156(3) के तहत याचिका दाखिल करते समय, हमने पहले कहा है कि धारा 154(1) और 154(3) के तहत पहले भी आवेदन किए गए होंगे।
इसी तरह, पटना उच्च न्यायालय ने योगेश मल्होत्रा बनाम बिहार राज्य (2017) और बिपिन कुमार सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2016) में कहा कि, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 (1) और (3) के अनुपालन के अभाव में एक शिकायतकर्ता संहिता की धारा 156 (3) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्देश मांगने के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर सकता है।
सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत की गई जांच धारा 202 के तहत निर्देशित जांच से कैसे अलग है
संहिता की धारा 156 पुलिस कर्मियों की जांच करने की शक्तियों से संबंधित है; धारा 202 की अवधारणा धारा 156 से भिन्न है। धारा 202 द्वारा प्रदान किया गया अधिकार विशिष्ट है।
उपरोक्त नियम के तहत मांगी गई रिपोर्ट का उद्देश्य केवल यह निर्धारित करना है कि “कार्यवाही के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।” यदि यह प्रत्याशित परिणाम है तो धारा 157 या 173 के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाना चाहिए।
धारा 157 के अनुसार, पुलिस को किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी की सूचना देनी चाहिए जिसके बारे में जानने के बाद उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है। पुलिस को घटनास्थल पर जाना चाहिए, सूचना की जांच करनी चाहिए और गिरफ्तारी करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तब पुलिस को मजिस्ट्रेट के लिए धारा 190 के तहत कार्य करने के लिए किसी भी बयान और रिपोर्ट का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। यह प्रक्रिया केवल तभी लागू होती है जब पुलिस कानून द्वारा दंडनीय अपराध पर जानकारी प्राप्त करती है, मामला दर्ज करती है और आवश्यक राय बनाती है।
संहिता के अध्याय XII में “पुलिस को सूचना और जांच करने के उनके अधिकार” से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। शिकायत पर किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले, उसके दौरान और बाद में एक मजिस्ट्रेट को जो कार्रवाई करनी चाहिए, वह अध्याय XV में शामिल है, जिसमें धारा 202 भी शामिल है।
ऊपर वर्णित दो अध्यायों के प्रावधान दो अलग-अलग पहलुओं से निपटते हैं, एक सामान्य तत्व की संभावना के बावजूद जैसे दोनो मामलो में एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत। पुलिस कर्मियों की संज्ञेय अपराधों की जांच करने की क्षमता अध्याय XII की धारा 156 में शामिल है। जैसा कि धारा 202 में कहा गया है, एक मजिस्ट्रेट “एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच का निर्देश दे सकता है”।
हालाँकि, धारा 202 द्वारा परिकल्पित जाँच संहिता की धारा 156 द्वारा परिकल्पित जाँच से अलग है। अध्याय XII में संहिता की धारा 156 के तहत जांच के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। एक थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली एक डायरी का उपयोग इस तरह की जांच की शुरुआत में एक संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में प्रासंगिक जानकारी के सार को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाएगा।
संहिता की धारा 173 के अनुसार, उसके बाद शुरू की गई जांच को पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके ही पूरा किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना भी पुलिस उस अध्याय में परिकल्पित जांच शुरू कर सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि धारा 156(3) के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित जांच अलग होगी। केवल संहिता की धारा 173 में परिकल्पित रिपोर्ट ही इस तरह की जांच का निष्कर्ष निकाल सकती है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक मजिस्ट्रेट को अध्याय XII के तहत जांच का आदेश देने से पहले अपराध का संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि, यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेने की योजना बनाता है, तो उसे ऐसी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। उल्लंघन के बारे में पता चलने के बाद, उसे संहिता के अध्याय XV में बताए गए चरणों का पालन करना चाहिए। संहिता की धारा 202(1) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसमें उल्लिखित जांच सीमित है।
मजिस्ट्रेट इस तरह की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी सहित किसी को भी आदेश दे सकता है। इस तरह की जांच मजिस्ट्रेट को यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि क्या उसके आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त औचित्य है। धारा 202(1) की अंतिम पंक्तियाँ, “या एक पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जांच की आवश्यकता होती है, जिसे वह उचित समझे, यह तय करने के लिए कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं,” यह स्पष्ट करती है।
न्यायिक घोषणाएं
- मधुबाला बनाम सुरेश कुमार (1997), के निर्णय के अनुसार एक मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(a) के तहत एक अपराध का संज्ञान ले सकता है या अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत प्राप्त करने के बाद धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच का आदेश दे सकता है। हर बार जब कोई मजिस्ट्रेट किसी शिकायत की जांच का आदेश देता है, तो पुलिस को शिकायत को प्राथमिकी मानते हुए एक संज्ञेय मामला दर्ज करना चाहिए। धारा 156(3) के तहत इस तरह का निर्देश मिलने के बाद, पुलिस को धारा 156(1) के तहत शिकायत की जांच करनी चाहिए। जांच पूरी होने के बाद, उन्हें धारा 173(2) के तहत एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिस पर एक मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(a) के बजाय धारा 190(1)(b) के तहत अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।
- श्रीनिवास गुंदलूरी और अन्य बनाम मैसर्स एसईपीसीओ इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और अन्य (2010), में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आदेश देकर, मजिस्ट्रेट ने बिना यह विचार किए कि क्या ऐसा करने का कोई वैध आधार था, शिकायत को अपना लिया था। उसने धारा 200 के तहत शिकायत या उसके गवाहों से पूछताछ करके संहिता के अध्याय XV को लागू नहीं किया था। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच करने, आरोप पत्र दायर करने, या अंतिम रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देकर अपने अधिकार में काम किया है। इस उदाहरण में, प्रतिवादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अपीलकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। धारा 156(3) के तहत उनका आवेदन मंजूर होने के बाद मूल शिकायत को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया गया था। उचित जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करने और आरोप पत्र पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था।
- माधव राव बनाम महाराष्ट्र राज्य (1971) में, यह कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के पास एक निजी शिकायत के रूप में धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज किए जाने पर भी जांच का आदेश देने का अधिकार था। मजिस्ट्रेट को केवल धारा 200 के तहत प्रस्तुत की गई शिकायत का तुरंत जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक निजी शिकायत है। मजिस्ट्रेट के पास यह निर्णय लेने का विकल्प है कि संज्ञान लिया जाए या नहीं। धारा 200 अपने आप में एक पूर्व-संज्ञान चरण है। इस प्रकार मजिस्ट्रेट पुलिस जांच का आदेश देने के लिए स्वतंत्र है या मजिस्ट्रेट खुद जांच करवा सकता है। इस पूछताछ या जांच के बाद, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जाए या नहीं। मजिस्ट्रेट केवल इस तरीके से कार्य कर सकता है, अर्थात, संज्ञान लेने से पहले वैकल्पिक उपाय की तलाश कर के।
- रमेश भाई पांडुराव हेडाऊ बनाम गुजरात राज्य (2010) में, यह निर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 156(3) और 202 मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश देने का अधिकार देती है। पूर्व-संज्ञान तब होता है जब धारा 156(3) के तहत शक्ति का उपयोग किया जाता है, लेकिन पश्च-संज्ञान तब होता है जब धारा 202 के तहत इसी तरह की जांच करने के अधिकार का उपयोग किया जाता है। मजिस्ट्रेट ने, इस मामले में, बाद के दृष्टिकोण का पालन करने का फैसला किया और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत विरोध याचिका को संहिता की धारा 200 के तहत एक शिकायत के रूप में माना। परिणामस्वरूप, उन्होंने धारा 202 के तहत कार्यवाही की और मामले के तथ्यों की जांच के लिए मामले को बरकरार रखा। मजिस्ट्रेट ने मामले को कैसे संभाला, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मान लीजिए धारा 202(2) के तहत मजिस्ट्रेट को यह उचित लगता है। वह या तो धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज कर सकता है या धारा 193 के तहत एक प्रस्ताव बना सकता है और मामले को सत्र न्यायालय में भेज सकता है।
- अशोक ज्ञानचंद वोहरा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) में, यह निर्णय लिया गया कि विशेष न्यायालय के पास महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1991 की धारा 9 और 23 के तहत एक संगठित अपराध के किए जाने के बारे में एक निजी शिकायत प्राप्त करने के बाद धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया था कि धारा 23(2) के तहत एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के लिए प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है।
- सुरेंद्र नाथ स्वैन बनाम उड़ीसा राज्य (2005) में आयोजित किया गया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत नियुक्त एक विशेष न्यायाधीश सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दी गई परिभाषा के तहत मजिस्ट्रेट नहीं है। इसलिए, वह जांच के लिए पुलिस को शिकायत नहीं भेज सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी बनाम वी. नारायण रेड्डी (1976) में फैसला सुनाया कि जब एक मजिस्ट्रेट शिकायत प्राप्त करता है। उसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वाक्यांश “ऐसी जांच का आदेश दे सकता है” प्रावधान की भाषा में यह स्पष्ट करता है कि मजिस्ट्रेट के पास विवेक है, जो मामले से मामले में भिन्न होता है। मजिस्ट्रेट को पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। नतीजतन, संहिता की धारा 154 और 156 (3) की भाषा में काफी अंतर है।
- रामदेव फूड प्रोडक्ट्स बनाम गुजरात राज्य (2015) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 156 (3) के तहत एक निर्देश केवल मजिस्ट्रेट के विचार के आवेदन के बाद ही दिया जाना चाहिए। केवल पूर्व-संज्ञान चरण में ही कोई मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दे सकता है। नतीजतन, अगर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने का फैसला करता है लेकिन न्यायाधीश धारा 190, 200, या 204 के तहत संज्ञान नहीं लेता है, तो मजिस्ट्रेट कानून द्वारा धारा 156(3) के तहत किसी भी जांच का आदेश देने के लिए अधिकृत नहीं है।
- स्किपर बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य (2001) में, यह निर्धारित किया गया था कि एक प्राथमिकी केवल वहीं दर्ज की जानी चाहिए जहां आगे की जांच आवश्यक हो या जब साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक हो जिसे शिकायतकर्ता संहिता की धारा 200 या 202 के तहत अदालत में पेश करने में असमर्थ था। इस बिंदु तक, अधिकांश भारतीय अदालतों ने हमेशा इस फैसले का अनुपालन किया है। संहिता की धारा 156(3) का निर्णय करने से पहले, एक मजिस्ट्रेट को निर्णय का प्रयोग करना चाहिए और ये निर्णय केवल शिकायतकर्ता के अनुरोध के आधार पर नहीं ले सकते है। इन शक्तियों का मुख्य रूप से उन स्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए जहां आरोप गंभीर हैं, शिकायतकर्ता साक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है, या किसी वस्तु को पुनर्प्राप्त करने या किसी कार्य को उजागर करने के लिए हिरासत सुविधा पूछताछ में आवश्यक प्रतीत होती है।
- अरविंदभाई रावजीभाई पटेल बनाम धीरूभाई संभूभाई (1997), में गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने संहिता की धारा 156(3) के तहत मामलों की जांच के लिए पुलिस को बुलाने की बढ़ती प्रथा पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त की और मजिस्ट्रेटों को तत्काल निर्णय न लेने की चेतावनी देते हुए फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेटों को संहिता की धारा 156(3) का उपयोग तभी करना चाहिए जब पुलिस की मदद अपरिहार्य (इंडिस्पेंसेबल) हो। मजिस्ट्रेट का मानना है कि अकेले शिकायतकर्ता दावों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा और पेश नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 202 के तहत, अगर शिकायतकर्ता को लगता है कि वह आवश्यक साक्ष्य जमा नहीं कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच करने और साक्ष्य पेश करने का आदेश दे सकता है, लेकिन वह कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। इस विषय पर उच्च न्यायालयों का रुख स्पष्ट रहा है: उनका मानना है कि प्राथमिकी केवल तभी दायर की जानी चाहिए जब कोई गंभीर अपराध किया गया हो या जब साक्ष्य किसी मान्यता प्राप्त अपराध के किए जाने को दर्शाते हो।
- फादर थॉमस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि एक संभावित प्रतिवादी के पास दोषी पाए जाने या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से पहले एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके धारा 156 (3) जांच आदेश पर विवाद करने का अधिकार नहीं है। यह मानते हुए कि संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने वाले इस तरह के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका अनुचित थी, पूर्ण पीठ ने कहा कि अभियुक्त को केवल मुकदमे के दौरान अपना बचाव पेश करने का अधिकार है। शिकायत दर्ज करने पर भी, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ता है, सम्मन जारी होने के बाद संभावित अभियुक्त को हस्तक्षेप करने या अपना मामला पेश करने की अनुमति नहीं होती है।
- के. विजया लक्ष्मी बनाम के. लक्ष्मीनारायण और अन्य (2000), में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह ध्यान रखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने इस मामले में धारा 156(3) के तहत कार्रवाई की और फिर पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने पर, संहिता की धारा 198 के तहत प्रावधानों की अनदेखी करते हुए, ऐसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया गया। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के अनुसार, मजिस्ट्रेट को उस अपराध का संज्ञान लेने की अनुमति नहीं है जो आईपीसी की धारा 494 का उल्लंघन करता है, जब तक कि शिकायतकर्ता, जिसने अपराध को नुकसान पहुंचाया है, औपचारिक शिकायत नहीं करता है। इस मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता, अभियुक्त नंबर 1 की पत्नी है, जिसे अभियुक्त 1 और 2 द्वारा किए गए अपराध के कारण गलत ठहराया गया था। संहिता की धारा 198(1)(c) के अनुसार, वास्तव में शिकायतकर्ता की शिकायत या उसकी ओर से की गई शिकायत के कारण अपराध को अपराध के रूप में मान्यता दी जा सकती थी। इस खंड को देखते हुए, मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किए गए पुलिस आरोप पत्र के आधार पर उल्लंघन को मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- यह पोलावरापू जगदीश्वरराव बनाम कोंडापटुरी वेंकटेश्वरलू (1990) के मामले में निर्धारित किया गया था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत शिकायत प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ बयान दर्ज करेगा, यदि कोई मौजूद है और धारा 190(1)(a) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और प्रक्रिया जारी कर सकता है, या धारा 202 के तहत प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत, मजिस्ट्रेट एक स्वतंत्र जांच कर सकता है या पुलिस जांच का आदेश दे सकता है। मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने या जारी करने में देरी भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट अपने विवेक का प्रयोग करते हुए शिकायत, शिकायतकर्ता के शपथ कथन, और गवाहों से किसी भी रिकॉर्ड की गई गवाही, यदि कोई हो, की जांच करता है और फिर तय करता है कि धारा 190(1)(a) के तहत अपराध का संज्ञान लेना है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत सम्मन जारी करना स्थगित करना है, या मामले को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस जांच के लिए को भेजना है। यदि वह यह निर्धारित करता है कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त है, तो वह धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच के लिए मामला भेज सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा यह निर्णय लेने के बाद कि वह शिकायत, शपथ कथनों और अन्य साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद अपराध का संज्ञान ले सकता है, धारा 156(3) लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- रसिकलाल दलपतराम ठक्कर बनाम गुजरात राज्य (2009) में, यह निर्णय लिया गया कि, जब तक कि बहुत विशेष और असामान्य परिस्थितियां न हों, मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर धारा 156(1) के तहत अधिकार वाले एक पुलिस अधिकारी को एक जांच करनी चाहिए। क्योंकि अपराध जांच एजेंसी के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया था, वह इसकी जांच करना बंद नहीं कर सकती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम प्रकाश पी. हिंदुजा और अन्य (2003) में कहा कि एक मजिस्ट्रेट पुलिस जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालांकि, इस फैसले का अनुपात तभी प्रासंगिक होगा जब पुलिस पूरी तरह से जांच करेगी। मजिस्ट्रेट उचित जांच करने के लिए पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को आदेश दे सकता है और आगे की निगरानी कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा नहीं किया गया है या धारा 156(3) के तहत एक आवेदन प्राप्त करने के बाद नहीं किया जा रहा है ( हालांकि उन्हें स्वयं जांच नहीं करनी चाहिए)।
- नवकिरण बनाम पंजाब राज्य (1995) में, याचिकाकर्ता और 16 अन्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र संबोधित किया जिसमें अधिवक्ताओं के अपहरण की घटनाओं और उनकी सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। रणबीर सिंह मंसतिया, जगविंदर सिंह और कुलवंत सिंह, जिनमें से सभी वकील थे, जिनका अपहरण कर लिया गया था, के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पत्र को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका के रूप में माना। इसने सीबीआई को अपहरण की जांच करने और उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
- सुभाष कृष्णन बनाम गोवा राज्य (2012) में, शिकायतकर्ता ने खुद को जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) के लिए पेश नहीं किया क्योंकि इस तरह के अपराध की ऐसी जांच टेलीफोन सूचना और उस व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई एक विस्तृत शिकायत के आधार पर शुरू हुई जिसे पुलिस पक्ष द्वारा लाया गया था जिसे घटना स्थल पर भेजा गया था। शिकायत की वजह से एक कार और हथियार के साथ अभियुक्त को पकड़ लिया गया। शिकायतकर्ता और कई गवाहों ने शिकायत के आधार पर अभियोजन मामले का समर्थन किया। यह माना गया था कि ऐसी परिस्थितियों में अभियोजन के मामलों को केवल इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता है क्योंकि शिकायतकर्ता से जिरह नहीं की जा सकती है।
- पी सिराजुद्दीन बनाम मद्रास राज्य (1970) में अभियोजन पक्ष के गवाहों को क्षमा करने वाले जांच अधिकारी के रूप में दो लोगों से पूछताछ की जानी थी। यह निर्णय लिया गया कि संहिता अभियोजन से प्रतिरक्षा को मान्यता नहीं देती है और पुलिस अधिकारियों के पास क्षमादान देने का विवेकाधिकार नहीं है।
- हसन अली खान बनाम राज्य (1991) में, यह निर्णय लिया गया था कि यदि प्राथमिकी और अन्य सामग्री, जैसे आरोप पत्र, किसी भी अपराध की पहचान करने में विफल रहती है, यदि कार्यवाही बेईमानी से शुरू की गई थी, या यदि कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करने का इरादा था, तो कार्यवाही आगे नहीं बढ़नी चाहिए। निहित अधिकार के तहत धारा 482 के तहत, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रोक सकता है।
- परमिंदर कौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2009) में, शिकायतकर्ता ने एक वृद्ध महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। आरोपों को अदालत द्वारा दुर्भावनापूर्ण और प्रतिशोधी माना गया। निर्णय लिया गया कि शिकायतकर्ता के पास वृद्ध महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कोई वैध कारण नहीं था। चिंतित जांच अधिकारी ने जांच प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और वृद्ध महिला के खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर दिया। हिरासत में लिए जाने के बाद, वृद्ध महिला को एक सप्ताह से अधिक समय जेल में बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह के एक मामले की जांच और विचारण न्यायालय द्वारा एक नाजायज अपराध की स्वत: मान्यता पर नाराजगी व्यक्त की। अभियोजन मामले को फलस्वरूप बाहर कर दिया गया क्योंकि यह कानूनी प्रणाली का दुरुपयोग करने के लिए निर्धारित किया गया था।
- यह जमुना बनाम बिहार राज्य (1966) में आयोजित किया गया था कि जांच अधिकारियों का कर्तव्य केवल अभियोजन पक्ष के मामले को ऐसे सबूतों के साथ मजबूत करना नहीं है, जो अदालत को सजा दर्ज करने में सक्षम बना सकते हैं, बल्कि पूर्ण वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) सत्य को सामने लाना है।
- एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की कि उसे भगवान सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1975) में रिश्वत की पेशकश की गई थी। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। शिकायतकर्ता ने खुद इसे एक दोष के रूप में देखा जो अनिवार्य रूप से अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य (1993) के मामले में एक पेशेवर वकील, उनकी पत्नी और उनके 2 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा अपनी जाँच समाप्त करने के बाद आरोप पत्र जारी किया गया था, लेकिन कानूनी समुदाय असंतुष्ट था और अदालती जाँच चाहता था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष अनुमति याचिका में कहा कि वे आम तौर पर जांच पूरी होने और आरोप पत्र दायर होने के बाद फिर से नहीं खोलेंगे। हालाँकि, उपयुक्त परिस्थितियों में, कानून को संतुष्ट करने और जनता के विश्वास को पूरी तरह से प्रेरित करने के लिए मामले को आगे की जाँच के लिए अधिकृत किया जा सकता है।
- प्राथमिकी केवल अपराध किए जाने की सूचना की एक रिपोर्ट है; यह ठोस साक्ष्य नहीं है क्योंकि पुलिस ने अभी तक उल्लंघन की जांच नहीं की है, यह सोहन लाल बनाम पंजाब राज्य (2003) में फैसला सुनाया गया था।
- राजस्थान राज्य बनाम किशोर (1996) में यह निर्णय लिया गया कि अभियोजन पक्ष के मामले को जांच अधिकारी की एक अनियमितता या अवैधता से प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, न ही उस आधार पर दोषमुक्ति दर्ज करने के लिए भरोसेमंद और विश्वसनीय साक्ष्य की अवहेलना की जा सकती है।
- के चंद्रशेखर बनाम केरल राज्य (1998) में, राज्य सरकार ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत दंडनीय अपराधों वाले एक मामले की जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी दी। सीबीआई ने अपनी जांच समाप्त की और एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सरकार ने तब अनुमोदन रद्द कर दिया और अनुरोध किया कि राज्य पुलिस घटना की अधिक गहन जांच करे। यह तय किया गया था कि चूंकि किसी भी आगे की जांच शुरू होने से पहले ही अभियुक्त का दोष निर्धारित किया जा चुका था – और यह एक ऐसे समय में जब अपराध का कमीशन अभी भी स्थापित करने की आवश्यकता थी – यह स्पष्ट था कि जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती और न ही होगी। इसका निष्कर्ष अपरिहार्य है। राज्य सरकार का यह कथन कि वह सहमति वापस ले रही है, प्राधिकरण के अनुचित उपयोग पर अमान्य हो सकती है।
- कुंगा नीमा लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य (2010) में, यह बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने पहले आपराधिक मामले की जांच से संबंधित उपचारों को सम्मानित किया था। रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग एक बार जारी जांच के विकास को ट्रैक करने या मौजूदा पूछताछ को एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में स्थानांतरित करने के लिए किया गया है। ऐसे निर्देश तब दिए गए हैं जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन स्पष्ट है, जो एजेंसी की निष्क्रियता या अन्य बातों के अलावा उदासीनता का परिणाम हो सकता है। जांच प्रक्रिया में विशिष्ट बाधाएं, जैसे कि गवाहों को ठोस खतरा, सबूतों को नष्ट करना, या शक्तिशाली हितों से अत्यधिक दबाव, रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से न्यायिक भागीदारी की मांग करते हैं। इनमें से किसी भी स्थिति में, रिट अदालतें केवल एक सुधारात्मक उपाय के रूप में कार्य कर सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जाँच की वस्तुनिष्ठता खतरे में न पड़े। हालांकि, एक रिट अदालत के साथ जांच शुरू करना व्यावहारिक नहीं है। यह जिम्मेदारी कार्यकारी शाखा की है, और यह जांच एजेंसियों पर निर्भर है कि वे यह निर्धारित करें कि उनके सामने रखी गई जानकारी जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त औचित्य है या नहीं। प्रथम दृष्टया के न्यायालयों को चल रही जाँचों पर कुछ नियंत्रण रखने के लिए संहिता में कुछ अधिकार दिए गए हैं। रिट अदालतों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों के बिना आपराधिक जांच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है क्योंकि वैधानिक कानून विचारण न्यायालय द्वारा कार्रवाई की गुंजाइश को विनियमित करते हैं।
- करण सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2013) में, यह निर्णय लिया गया था कि जांच में त्रुटियां केवल अभियोजन की कार्यवाही के लिए घातक हैं यदि वे इतनी गंभीर हैं कि पूरी जांच की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया जा सकता है। जांच की अस्पष्ट प्रकृति और अधिकारी के खिलाफ गंभीर अनुचितता के निष्कर्षों के बावजूद, सरकार ने कुछ नहीं किया। नतीजतन, सरकार को कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वीके मिश्रा बनाम उत्तराखंड राज्य (2015) में फैसला सुनाया कि “जांच अधिकारी को उस दृष्टिकोण से सभी संभावित बचावों और जांच का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है।” किसी भी मामले में, जांच अधिकारी की किसी भी निगरानी को अभियोजन पक्ष के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्याय की आवश्यकता है कि जांच अधिकारी के इन कार्यों या निष्क्रियताओं को अभियुक्त के पक्ष में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना उन कार्यों को पुरस्कृत करने के बराबर होगा।
निष्कर्ष
सीआरपीसी की धारा 156, 190, 200 और 202 मजिस्ट्रेट की शक्तियों और जांच के आदेश देने, संज्ञान लेने, आरोप लगाने आदि के लिए उनके विकल्पों का विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं।
मजिस्ट्रेट, हालांकि, जांच का आदेश दे सकता है, संज्ञान ले सकता है, आरोपों का मसौदा तैयार कर सकता है आदि, भले ही मजिस्ट्रेट के पास धारा 156 (3) के तहत पूर्व-संज्ञान चरण में जांच का आदेश देने का अधिकार हो, भले ही एक आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट एक बार जमा करने के बाद संज्ञान लिया जाता है।
इसी के तहत अभियुक्त पेश होता है। उसके पास स्वत: संज्ञान लेने या शिकायतकर्ता के अनुरोध या प्रार्थना पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त जांच का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं होता है। हालांकि यह संज्ञान के बाद की अवस्था में है, यह यह निर्धारित करने के लिए एक जांच की तरह है कि क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। इस तरह के एक जांच निर्देश संहिता की धारा 173(8) द्वारा परिभाषित आगे की जांच का गठन नहीं करता है।
इसलिए, सीआरपीसी की धारा 156(3) एक मजिस्ट्रेट को उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी अधिकार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने और एक औपचारिक जांच करने की शक्ति शामिल है, यदि मजिस्ट्रेट आश्वस्त हो जाता है कि पुलिस ने उचित जांच नहीं की है या नहीं कर रही है।
हालांकि संक्षेप में कहा गया है, संहिता की धारा 156(3) यथोचित रूप से व्यापक है और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी आकस्मिक शक्तियों को शामिल करती है।
अंत में, यह सुझाव दिया जा सकता है: –
- सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत काम करने वाले मजिस्ट्रेट, मामले (प्राथमिकी) के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) और उसके बाद की जांच का आदेश देने के लिए सक्षम होंगे।
- मजिस्ट्रेट, आदेश पारित करते समय, दिमाग का प्रयोग करके कार्य करते हैं, जो कि आदेश में परिलक्षित होना चाहिए।
- शिकायतकर्ताओं को जिम्मेदार बनाने के लिए धारा 156 (3) के तहत एक शपथ पत्र आवेदन प्रदान करने के लिए सीआरपीसी में संशोधन किया जाए।
- पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने के बजाय मजिस्ट्रेट शिकायतों की सत्यता और वास्तविकता का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकते हैं।
- लोक सेवकों से जुड़े मामलों में, मजिस्ट्रेट को केवल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश पारित करने चाहिए, यदि अभियोजन पक्ष धारा 197(1) के तहत वैध मंजूरी देता है।
- प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के संबंध में, मामला लिखने से पहले शिकायत की सत्यता के बारे में विस्तृत जांच की जाती है ताकि तंग करने वाले मुकदमों से बचा जा सके।
- मजिस्ट्रेटों को केवल योग्य मामलों को ही पुलिस जांच के लिए भेजना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
“संज्ञान लेना” मुहावरे का क्या अर्थ है?
आपराधिक प्रक्रिया संहिता “संज्ञान लेने” को परिभाषित नहीं करती है। संहिता की धारा 190(1)(a) के तहत कार्रवाई करने के लिए, एक मजिस्ट्रेट को न केवल याचिका की सामग्री पर विचार करना चाहिए बल्कि अतिरिक्त जांच के लिए शिकायत को अग्रेषित (फॉरवर्ड) करने से पहले एक विशिष्ट कार्रवाई का पालन करने के इरादे से ऐसा करना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत, एक मजिस्ट्रेट भी जांच का आदेश दे सकता है।
अगर पुलिस थाना प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दे तो किसी को कैसे जवाब देना चाहिए?
पुलिस थाने को कानून द्वारा दंडनीय किसी भी अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त या या पुलिस आयुक्त को सूचना के सार के साथ मेल द्वारा संपर्क किया जा सकता है यदि पुलिस थाने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करता है। अगर वह आश्वस्त है कि सूचना कानून द्वारा दंडनीय अपराध का खुलासा करती है, प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, और एक जांच शुरू की जानी चाहिए। आप आरटीआई दर्ज कर सकते हैं, राज्य के गृह मंत्रालय को एक शिकायत, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट के पास एक निजी शिकायत, या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक सतर्कता/ भ्रष्टाचार-विरोधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं की गई है।
क्या अदालत से अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी पुलिस किसी को जांच के लिए बुला सकती है?
निश्चित रूप से हां। न्यायालय केवल गिरफ्तारी पर रोक लगाता है; पुलिस अभी भी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। यह लगभग हमेशा अग्रिम जमानत की आवश्यकता होती है कि जांच अधिकारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर अभियुक्त खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराए। यदि प्रतिवादी इनकार करता है तो जांच अधिकारी अदालत से अग्रिम जमानत रद्द करने का अनुरोध कर सकता है। भले ही अपराध गैर-जमानती हो, अगर जांच अधिकारी यह निर्धारित करता है कि जिस अभियुक्त को अदालत ने अग्रिम जमानत दी है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला बनाया गया है, तो वह उसे गिरफ्तार नहीं करेगा बल्कि जमानत पर रिहा कर देगा।
संदर्भ
- SN Mishra, The Code of Criminal Procedure, 22nd Edition (2020), Pg.234-246
- RV Kelkar’s Criminal Procedure, 7th Edition (2021), Pg.132-136
- Ratanlal & Dhirajlal, The Code of Criminal Procedure, 22nd Edition (2017), Pg.288-302