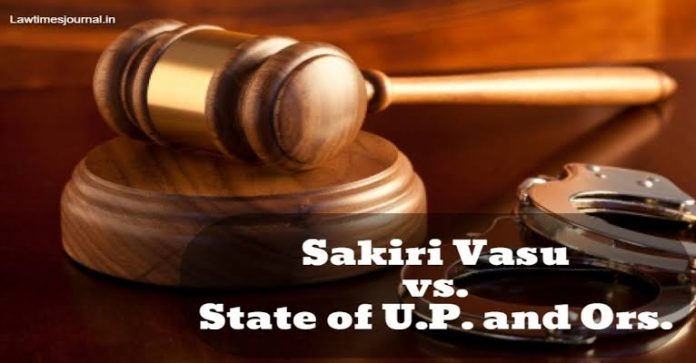यह लेख Shahela द्वारा लिखा गया है। यह लेख साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले के माध्यम से, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस की भूमिका और शक्ति और सीआरपीसी की धारा 156 के तहत जांच की निगरानी करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति का विस्तार से विश्लेषण करना चाहता है। इसके अलावा, लेख इस मामले में चर्चा किए गए कानूनों और मिसालों के साथ-साथ निहित शक्ति के सिद्धांतों और क़ानूनों के निर्माण को अद्यतन (अपडेट) करने से संबंधित है। रिट याचिका पर विचार करने और उसकी रखरखाव की उच्च न्यायालय की शक्ति का विश्लेषण करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2007) का मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेखनीय निर्णयों में से एक है। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद सीआरपीसी के रूप में संदर्भित) की धारा 156(3) के महत्व और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित है और चर्चा करता है। सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्रावधानों का दायरा बेहद व्यापक है। इस मामले के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत अधिकार देकर पुलिस को उचित जांच और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का निर्देश दिया, जो कि इस मामले में पहले नहीं किया गया था।
सीआरपीसी की धारा 154(1) के अनुसार, यदि संज्ञेय अपराध की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी को थाने में मौखिक रूप से दी जाती है, तो वह पुलिस अधिकारी उस सूचना को स्वयं या उसके निर्देशन में अपने किसी अधीनस्थ द्वारा लिखवाने के लिए उत्तरदायी होता है, जिस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के साथ-साथ स्वयं भी हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद, शिकायत सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेज दी जाएगी। लिखित में शिकायत मिलने पर एसपी शिकायत की सत्यता की जांच करेंगे और यदि शिकायत संज्ञेय अपराध की विशेषताओं का खुलासा करती है, तो जांच स्वयं की जाएगी या सीआरपीसी के तहत निर्धारित तरीके से जांच के लिए निर्देश उसके किसी अधीनस्थ को दिया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को उन संज्ञेय (कॉग्निजेबल) मामलों को देखने की शक्ति प्रदान की गई है जहां सीआरपीसी की धारा 190 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को जांच के निर्देश दिए जाते हैं।
किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए शिकायत करने वाले व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा मामले की उचित जांच के लिए सीआरपीसी में उपर्युक्त प्रक्रिया उपलब्ध है। सबसे पहले, शिकायत को लिखित रूप में दर्ज करना है, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा मौखिक रूप से किया गया है। यदि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करने में कोई विफलता होती है, तो शिकायतकर्ता लिखित आवेदन के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत एसपी तक पहुंच सकता है। और अगर एसपी भी शिकायत दर्ज नहीं करता है, तो शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास पहुंच कर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और मामले की उचित जांच के लिए निर्देश दे सकता है।
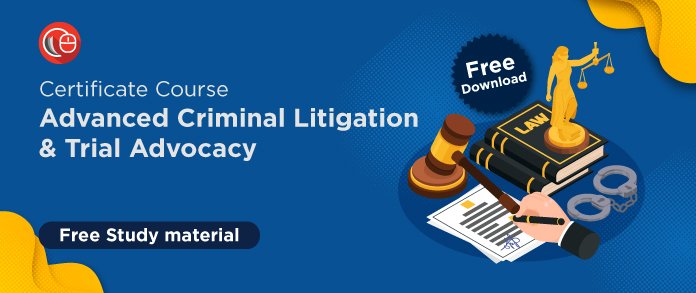
साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) का विवरण
- मामले का नाम: साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
- मामला संख्या: अपील (सीआरएल) 1685, 2007
- समतुल्य उद्धरण: 2007 एससीसी ऑनलाइन एससी 1488 या (2008) 2 एससीसी 409
- शामिल अधिनियम: भारत का संविधान, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946।
- महत्वपूर्ण प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 32, 136 और 226; धारा 154 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 36, 156(3), 200, और 482 के साथ पठित; और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 3।
- न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय
- खंडपीठ: 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ; ए.के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.
- याचिकाकर्ता: साकिरी वासु
- प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
- निर्णय दिनांक: 07/12/2007
जांच की निगरानी करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां
सीआरपीसी की धारा 156 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को उचित जांच के लिए निर्देश देने की शक्ति है। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की निगरानी करने की इस शक्ति के कुछ चरण हैं, जिन्हें नीचे समझा जा सकता है:
- पहला चरण एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस को जांच के लिए निर्देशित करना है।
- दूसरा चरण वह है जहां जांच की प्रक्रिया में व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी की वैधता निर्धारित करने और गिरफ्तारी की श्रेणी, न्यायिक या पुलिस तय करने के लिए उसे 24 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।
- तीसरा चरण सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेप है, जहां एक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने बयान देता है और साथ ही आईडी सत्यापन, पहचान और आवेदन मांगता है।
- चौथा चरण है जांच की निगरानी।
- पांचवां चरण एफआईआर दर्ज होने के बाद सीआरपीसी की धारा 173 के तहत आगे की जांच का निर्देश है।
साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) के तथ्य
यह अपील आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 9308/2007 में 13.07.2003 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश और फैसले के खिलाफ व्यथित याचिकाकर्ता द्वारा पारित की गई थी। याचिकाकर्ता का एस. रविशंकर नाम का एक बेटा है, जो भारतीय सेना में मेजर था। उनका शव 23.08.2003 को मथुरा रेलवे स्टेशन पर मिला था। राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.), मथुरा ने मृतक के मामले की जांच की और 29.08.2003 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और निष्कर्ष निकाला कि यह या तो एक दुर्घटना थी या आत्महत्या थी।
पूछताछ के दौरान न्यायालय ने सहायक (घरेलू नौकर) और मुख्य चश्मदीद राम स्वरूप के बयानों पर भरोसा किया। सहायक (घरेलू नौकर) ने बयान दिया कि मेजर एस. रविशंकर कभी भी खुशमिजाज़ व्यक्ति नहीं थे, वह बरामदे में कुर्सी पर बैठे रहते थे और हमेशा अलग, सूनी आँखों से छत की ओर देखते थे। वह हमेशा किसी गहरे विचार में डूबा रहता था और अपने आस-पास के माहौल से अनजान रहता था। प्रत्यक्षदर्शी गैंगमैन राम स्वरूप ने बताया कि मेजर रविशंकर दिल्ली की ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। लेकिन मृतक के पिता को अपने बेटे की मौत पर संदेह था और उन्होंने दावा किया कि यह आत्महत्या के बजाय हत्या है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें सेना की मथुरा इकाई में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया था और उन्होंने इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक इसी वजह से उनके बेटे की हत्या कर दी गयी।
इस मामले की पहली अदालती जांच सेना ने की थी, जिसने 2003 में अपनी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या का मामला बताया था। रिपोर्ट से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने 24.04.2004 को तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल एन.वी. विज से एक और विस्तृत जांच की मांग की, लेकिन रिपोर्ट का निष्कर्ष वही था, जिसमें मामले को आत्महत्या बताया गया। सेना न्यायालय की दोनों जांचों से व्यथित याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की प्रार्थना की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति द्वारा यह अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी।
उठाये गये मुद्दे
- क्या मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत सीबीआई से जांच का आदेश पारित करने की शक्ति है?
- क्या मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश को खारिज करने की शक्ति है?
- क्या सीआरपीसी में वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने पर भी कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है?
- क्या पीड़ित पक्ष के लिए जांच के लिए किसी विशिष्ट एजेंसी की मांग करना संभव है?
- क्या मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत ‘अंतिम रिपोर्ट’ प्रस्तुत होने के बाद जांच को फिर से खोलने के आदेश को खारिज करने की शक्ति है?

साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) में पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता
- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के बेटे मेजर एस. रविशंकर को मथुरा आर्मी यूनिट में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में पता था। उन्होंने इसकी मौखिक शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की और अपने पिता को भी इस भ्रष्टाचार के बारे में सूचित किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बेटे की हत्या इसी कारण से की गई थी।
- याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि जीआरपी मथुरा द्वारा उचित जांच नहीं की गई, और उनके बेटे की मौत को आत्महत्या बताने वाली उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट दोषपूर्ण है।
- अंत में, याचिकाकर्ता जीआरपी मथुरा और सेना न्यायालयों द्वारा की गई जांच और पूछताछ से संतुष्ट नहीं था, उसने अपनी रिट याचिका में सीबीआई जांच के लिए प्रार्थना की।
प्रतिवादी
- उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि, सेना द्वारा की गई पूछताछ के अनुसार, सहायक (घरेलू सहायता) के बयान पर भरोसा करते हुए, मेजर एस रविशंकर कभी-कभी अपने परिवेश से अनजान रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जांच में पता चला कि मेजर एस रविशंकर की मृत्यु दुर्घटनावश हुई क्योंकि वह दिल्ली से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे। प्रत्यक्षदर्शी गैंगमैन रामस्वरूप ने भी यही देखा।
- प्रतिवादी द्वारा दिया गया तर्क यह था कि जीआरपी जांच ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के बेटे की मौत या तो एक दुर्घटना थी या आत्महत्या थी, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता जांच परिणामों से असंतुष्ट था, इसलिए राज्य द्वारा सेना न्यायालय को एक और जांच का आदेश दिया गया था।
- प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि कोई व्यक्ति विशेष रूप से किसी विशेष एजेंसी से जांच की मांग नहीं कर सकता है; इसके बजाय एक और जांच की मांग की जा सकती है।
साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) में कानून और उदाहरणों पर की गई चर्चा
मामले से संबंधित धाराएं और अनुच्छेद निम्नलिखित हैं
- सीआरपीसी की धारा 154(1): इस प्रावधान में कहा गया है कि पीड़ित व्यक्ति अपने खिलाफ हुए संज्ञेय अपराध की शिकायत पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी से कर सकता है। इसे उसके द्वारा या उसके आदेश पर किसी अन्य पुलिस द्वारा कम शब्दों में लिखा जाएगा और उसे शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाया जाएगा।
- सीआरपीसी की धारा 154(3): यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो पीड़ित एक आवेदन लिखकर पुलिस अधीक्षक (एसपी) से संपर्क कर सकता है। एसपी या तो खुद या अपने किसी मातहत (सबोर्डिनेट्स) को इसकी जांच करने का निर्देश देते हैं।
- सीआरपीसी की धारा 156(3): यदि उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है या उचित जांच नहीं की गई है तो पीड़ित व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत कर सकता है। मजिस्ट्रेट दोनों के लिए आदेश दे सकता है।
- सीआरपीसी की धारा 36: धारा 36 उन संबंधित पुलिस अधिकारियों के बारे में बात करती है जिनसे किसी प्रभारी अधिकारी या एसपी, यानी, डीआइजी, डीजीपी या आइजी के इनकार के मामले में शिकायत की जानी है।
- सीआरपीसी की धारा 200: किसी अपराध के पंजीकरण के लिए पीड़ित द्वारा मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत की जा सकती है।
- सीआरपीसी की धारा 482: न्याय बनाए रखने के लिए संहिता में कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आदेश पारित करना उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है।
- सीआरपीसी की धारा 173(8): यदि जांच अधिकारी को कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिलता है जो मामले की कार्यवाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबूत निर्धारित तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने रखे जाएंगे, और फिर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भी मजिस्ट्रेट को आगे की जांच के लिए आदेश पारित करने से कोई नहीं रोक सकता है।
- अनुच्छेद 136: यह विशेष क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है जिसके माध्यम से एक पीड़ित व्यक्ति विशेष अनुमति (एसएल) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है। इस प्रावधान के तहत किसी भी न्यायाधिकरण या न्यायालय के फैसले से व्यथित व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है। अनुच्छेद 136 के तहत एसएल देना सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है।
- अनुच्छेद 226: यह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है, जहां पीड़ित द्वारा रिट याचिका दायर की जा सकती है।
न्यायालय ने निर्णय सुनाने के लिए कई मामलो पर भरोसा किया।
सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य (2007)
इस मामले में, यह माना गया कि मजिस्ट्रेट के पास सीबीआई को जांच करने का आदेश देने की शक्ति नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। ऐसा केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाएगा, अन्यथा सीबीआई पर अनावश्यक मुकदमों का बोझ पड़ जाएगा और पुलिस की प्रासंगिकता में टकराव पैदा हो जाएगा।
सीबीआई बनाम राजेश गांधी और अन्य (1997)
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी इस मामले की जांच के लिए किसी विशेष एजेंसी की मांग नहीं कर सकता है। एक पीड़ित व्यक्ति को अपने द्वारा लगाए गए मामले की उचित जांच के लिए दावा करने का अधिकार है, लेकिन उसे अपनी पसंद की किसी विशिष्ट एजेंसी द्वारा की जाने वाली जांच के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।
मोहम्मद यूसुफ बनाम अफाक जहां और अन्य (2006)
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है। भले ही न्यायिक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत विशेष रूप से एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं देता है, फिर भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को शिकायतकर्ता द्वारा किए गए संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करनी होती है ताकि रिकॉर्ड का पता लगाया जा सके। अपराध के घटकों को पंजीकृत किया जा सकता है और उचित जांच की जा सकती है।

दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य (2007)
इस मामले में, मोहम्मद यूसुफ बनाम अफाक जहां के उपर्युक्त मामले के समान ही दृष्टिकोण इस मामले में न्यायालय द्वारा लिया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई हो और पुलिस द्वारा जांच कर ली गई हो या जांच जारी हो, अगर पीड़ित पक्ष इससे संतुष्ट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है। मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने के बाद उचित जांच का आदेश दे सकता है और कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है जिसे वह मामले की उचित जांच के लिए उपयुक्त समझता है।
बिहार राज्य बनाम जे.ए.सी. सलदान्हा (1980)
इस मामले में, मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आगे की जांच का आदेश देने की स्वतंत्र शक्ति है, जब सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच अधिकारी द्वारा जांच की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसलिए, यदि मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मामले को फिर से खोलने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है।
सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमन्त यशवन्त ढगे एवं अन्य (2010)
इस मामले में, यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की गई थी या उचित जांच नहीं की गई थी, तब पीड़ित व्यक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जो सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाना है।
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति
उच्च न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक अंतर्निहित शक्ति है, जो उच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने में सक्षम बनाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद यूसुफ बनाम अफाक जहां के मामले पर भरोसा किया। यह देखा गया कि भारत में उच्च न्यायालयों में एफआईआर दर्ज करने या उचित जांच के आदेश देने की प्रार्थना करने वाली रिट याचिकाओं की बाढ़ आ गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से ऐसी याचिकाओं पर विचार न करने को कहा और ऐसे मामलों को खारिज करने को कहा क्योंकि अन्य वैकल्पिक उपाय पहले से ही संहिता में मौजूद हैं। सबसे पहले, सीआरपीसी की धारा 154(3) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 36 के तहत पीड़ित पुलिस से संपर्क कर सकता है, और यदि ऐसी शिकायत को पुलिस अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, फिर, दूसरी बार, पीड़ित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रिट याचिका दायर करने के बजाय सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है, जिससे उच्च न्यायालय पर बोझ बढ़ जाएगा। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करने का उपाय भी उपलब्ध है।
साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) में चर्चा किए गए सिद्धांत
मामले में चर्चा किए गए कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं:
निहित शक्ति का सिद्धांत
यह पहले ही कहा जा चुका है कि जब किसी क़ानून द्वारा किसी प्राधिकरण को कोई शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान की जाती है, तो इसमें बिना किसी विशेष उल्लेख के चीजों को ठीक से करने के लिए निहित शक्तियां शामिल होती हैं। यदि ऐसी निहित शक्तियों से कोई इंकार या खंडन होता है, तो इसे उस प्रावधान के तहत अप्रभावी माना जाएगा। इसलिए, यदि कोई अधिनियम या क़ानून कोई व्यक्त शक्ति प्रदान करता है, तो ऐसा करने की निहित शक्ति पहले से ही दी गई है, और यह ऐसी शक्तियों के निष्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
क्रॉफर्ड ने अपने वैधानिक निर्माण में इस तरह के नियम का कारण व्यक्त करते हुए कहा, “...यदि इन विवरणों को निहितार्थ द्वारा सम्मिलित नहीं किया जा सका, तो कानून का मसौदा तैयार करना एक अंतहीन प्रक्रिया होगी, और विधायी मंशा संभवतः सबसे महत्वहीन चूक से पराजित हो जाएगी।”
सावित्री बनाम गोविंद सिंह रावत (1986) में, न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण-पोषण देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति का तात्पर्य मामला लंबित रहने के दौरान पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने की शक्ति से है।
उपर्युक्त कानूनी स्थिति पर विचार करने से, यह स्पष्ट है, जैसा कि धारा 156(3) में संक्षेप में कहा गया है, कि किसी आपराधिक अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने और मामले की उचित जांच के लिए पुलिस को निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की एक निहित शक्ति है। भले ही इन प्रक्रियाओं का सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी ये उपरोक्त प्रावधान में मजिस्ट्रेट की निहित शक्तियां हैं।
निर्माण को अद्यतन करने का सिद्धांत
निर्माण के सिद्धांत के अनुसार, कानून का विकास समाज के विकास के साथ-साथ होना चाहिए। नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन बनाम पी.आर. रामकृष्णन (1981) में माननीय न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि कानून स्थिर नहीं रह सकता; इसे सामाजिक मूल्यों और अवधारणाओं के साथ बदलने की जरूरत है। धारा 156(3) के अनुसार मामले को डाक के माध्यम से लिखित रूप में भेजा जाना आवश्यक है। तकनीकी उन्नति से पहले इसे संचार का सबसे तेज़ माध्यम माना जाता था। तकनीकी विकास के बाद, संचार के विभिन्न तरीके, जैसे व्हाट्सएप, ई-मेल, या सेलुलर कॉल, लिखित और पोस्ट के माध्यम से व्याख्या के लिए उपलब्ध हैं। जांच के ऐसे तरीकों को शामिल (कवर) करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाना चाहिए।

साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का निर्णय (2007)
सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई बनाम राजेश गांधी और अन्य के मामले पर भरोसा करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी न्यायालय के फैसले या पुलिस की जांच से व्यथित है, वह उचित जांच के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है लेकिन किसी निर्दिष्ट एजेंसी से जांच की मांग नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि जब कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद है, तो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे बोझ और मामलों की संख्या बढ़ जाएगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की, क्योंकि पहली नजर में सीबीआई द्वारा ऐसी जांच की अनुमति देने का कोई मामला नहीं था। जीआरपी मथुरा द्वारा की गई पिछली पूछताछ और सेना अधिकारियों द्वारा दो बार की गई जांच से पहले ही पता चला है कि मृतक की मौत का कारण दुर्घटना या आत्महत्या थी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि जांच की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करने की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसे मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया या नहीं। यदि रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाती है, तो मामला अभी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित माना जाता है, और कोई आदेश नहीं दिया गया है। यदि रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो मामला पूरा माना जाएगा।
फैसले के पीछे तर्क
माननीय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने कहा कि किसी व्यक्ति के सामने उच्च न्यायालय जाने के बजाय न्यायालय में वैकल्पिक उपाय मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुरुष या महिला को शिकायत करनी है, तो वे पुलिस स्टेशन से संपर्क करेंगे, और प्रभारी अधिकारी सीआरपीसी की धारा 154 (1) के तहत उनकी एफआईआर दर्ज करेंगे; यदि संपर्क से इनकार कर दिया गया, तो वे धारा 154(3) या धारा 36 के तहत पुलिस अधीक्षक (एसपी) का सहारा लेंगे। यदि शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रिट याचिका दायर करने के बजाय सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। इसके अलावा, व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 200 के तहत न्यायालय में आपराधिक शिकायत भी दर्ज कर सकता है।
यह पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रस्तुत एक वैकल्पिक उपाय है, लेकिन यह किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से नहीं रोकता है। रिट याचिका सीआरपीसी की धारा 482 और संविधान के अनुच्छेद 226 दोनों के तहत उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। हालाँकि, वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर उच्च न्यायालय याचिका को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) में न्यायालय की टिप्पणी और दिशानिर्देश
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:
- सीआरपीसी की धारा 154(1) के तहत शिकायत की सूचना पुलिस स्टेशन के प्रभारी कार्यालय को दें।
- यदि प्रभारी अधिकारी सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है, तो पुलिस अधीक्षक (एसपी) को रिपोर्ट करें।
- धारा 36 के तहत एसपी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यानी डीआइजी, डीजीपी, आइजी को रिपोर्ट करें।
- सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करने में विफलता के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने की शक्ति है।
- सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति।
- अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करें।

निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उल्लेखनीय ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए सीआरपीसी की धारा 154 और 156 के तहत एफआईआर दर्ज करने या उचित जांच के संबंध में अपने मुद्दों का सहारा लेने के लिए सीधे उच्च न्यायालयों या माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के बजाय व्यक्तियों के पास मौजूद वैकल्पिक उपायों के विचार का समर्थन किया है।
इस फैसले से यह स्पष्ट है कि, किसी भी उचित जांच के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। फिर मजिस्ट्रेट को मामले की आगे की उचित जांच का आदेश देने के लिए जांच अधिकारी द्वारा उसके सामने प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपराध का संज्ञान लेना चाहिए।
सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे और अन्य (2010) के हालिया फैसले में, यह निर्धारित किया गया था कि यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की गई है या उचित जांच नहीं की गई है, तो पीड़ित व्यक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, जो सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाना है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या उच्च न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रिट याचिका को खारिज करने की शक्ति है?
उच्च न्यायालय के पास सीआरपीसी की धारा 482 के तहत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करने की अंतर्निहित शक्ति है, खासकर जब कोई व्यक्ति निचली अदालतों के फैसले से असंतुष्ट हो। उच्च न्यायालय केवल उन मामलों में ऐसी याचिका पर विचार करेगा जहां कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद नहीं है, खासकर जब सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई थी और सीआरपीसी की धारा 156 के तहत उचित जांच नहीं की गई थी। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले, पीड़ित पक्ष के पास कई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होते हैं। इन उपायों में सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत पुलिस अधीक्षक से समस्या निवारण की मांग करना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 36 के तहत डीआइजी, डीजीपी और आइजी को संबोधित करना और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करना शामिल है।
क्या मजिस्ट्रेट के पास जांच दोबारा शुरू करने का अधिकार हो सकता है?
सीआरपीसी की धारा 178 के तहत मजिस्ट्रेट को दो स्थितियों में जांच अधिकारी को शिकायत की दोबारा जांच करने का आदेश देने का अधिकार है। पहला, अगर वह पुलिस द्वारा सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। दूसरे, अगर कोई नया ठोस सबूत सामने आया है।
संदर्भ
- Earl T Crawford, The Construction of Statutes 1008 (1940).