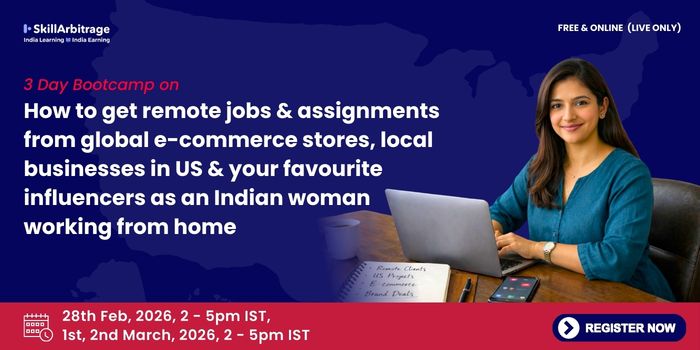यह लेख Satyanshu Kumari द्वारा लिखा गया है। यह लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत स्वीकृति (एडमिशन) और स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) की अवधारणाओं पर चर्चा करता है, जिसमें स्वीकृति और स्वीकारोक्ति दोनों अधिनियम के तहत अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। इस लेख में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 24 से धारा 30 के तहत विभिन्न प्रकार की स्वीकारोक्ति पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) का मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी मामला है जो आपराधिक मामलों में स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता पर गहनता से विचार करता है। यह मामला आपराधिक कानून और साक्ष्य कानून के अंतर्गत आता है, जो विशेष रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) (जिसे आगे ‘साक्ष्य अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 24 से 30 की व्याख्या और लागू करने पर केंद्रित है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अभियुक्त द्वारा स्वयं को दोषी ठहराने वाला बयान स्वीकारोक्ति माना जा सकता है, और क्या इस तरह के स्वीकारोक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार की आवश्यकता होती है, जो अदालत में स्वीकार्य हो।
स्वीकृति और स्वीकारोक्ति दोनों भारतीय साक्ष्य अधिनियम के श्रवण नियम के अपवाद हैं। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि स्वीकृति और स्वीकारोक्ति का प्रामाणिक (प्रोबेटीव) मूल्य (मुद्दे में किसी प्रासंगिक तथ्य के प्रमाण उद्देश्य तक पहुँचने की संभावना) एक दूसरे के आचरण पर निर्भर नहीं है, लेकिन, किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह, इसे केवल तभी साक्ष्य माना जा सकता है जब यह सिद्ध हो। यह प्रमाण केवल उन गवाहों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने स्वीकृति या स्वीकारोक्ति को सुना हो, जैसा भी मामला हो। इस लेख में, हम स्वीकृति और स्वीकारोक्ति को समझेंगे, जो साक्ष्य के श्रवण नियम के अपवाद हैं।
मामले का विवरण
- मामले का नाम- साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1966 एआईआर 40
- समतुल्य उद्धरण (साइटेशन)- 1966 एआईआर 40
- मामला संख्या: 1964 का 248
- शामिल अधिनियम: भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे “आईपीसी” कहा गया है) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872।
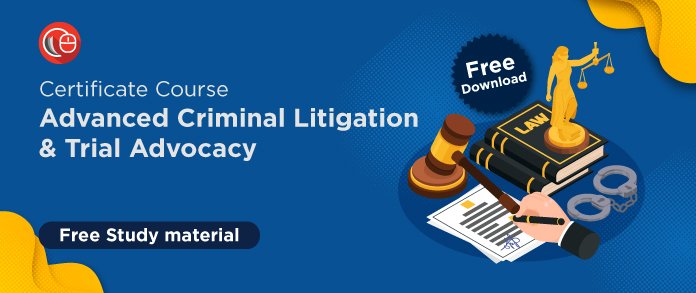
- प्रासंगिक क़ानून और प्रावधान: आईपीसी की धारा 302 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30।
- न्यायालय का नाम- भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- पीठ- न्यायमूर्ति सुब्बाराव के, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह और न्यायमूर्ति आर.एस. बछावत
- याचिकाकर्ता- साहू
- प्रतिवादी- उत्तर प्रदेश राज्य
- निर्णय की तिथि- 16 फरवरी 1965
साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) के तथ्य
- उक्त मामले में अपीलकर्ता साहू गोंडा जिले के पचपेरवा का निवासी है। उसके दो बेटे हैं, बद्री और कृपाशंकर। उसने कई साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था। उसके सबसे बड़े बेटे बद्री ने सुंदरपट्टी से शादी की थी। बद्री ने लखनऊ में नौकरी कर ली थी और इसलिए उसकी पत्नी उसके पिता, अपीलकर्ता के साथ रहती थी। आम तौर पर यह माना जाता था कि सुंदरपट्टी और साहू के बीच नाजायज संबंध थे जो अंतरंग थे।
- हालाँकि, उनके बीच कई बार झगड़े हुए और 12 अगस्त 1963 को ऐसे ही एक झगड़े के दौरान सुन्दरपट्टी भागकर अपने पड़ोसी मुहम्मद अब्दुल्ला के घर चली गई।
- अपीलकर्ता ऐसे ही एक झगड़े के बाद उसे वापस ले आया और कुछ सांसारिक तकरार के बाद वे दोनों घर के एक ही कमरे में सोये। अपीलकर्ता का दूसरा बेटा, कृपा शंकर, जो 8 साल का था, घर का एकमात्र निवासी था।
- अगली सुबह सुदरपट्टी गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, हालांकि कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई।
- उसी सुबह, अपीलकर्ता को अपने आप से यह कहते हुए देखा गया कि उसने सुदरपट्टी को समाप्त कर दिया है, उसने दैनिक झगड़ों को खत्म कर दिया है। साहू को आईपीसी की धारा 302 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 101, जिसे आगे “बीएनएस, 2023” कहा गया है) के तहत आरोप पर गोंडा के सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए भेजा गया था।
उठाए गए मुद्दे
- क्या अभियुक्त द्वारा बड़बड़ाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकारोक्ति के बराबर है और यदि हां, तो क्या यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के तहत यह स्वीकार्य साक्ष्य है?
- क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से 30 के अंतर्गत न्यायेतर स्वीकारोक्ति के लिए किसी अन्य व्यक्ति से संवाद आवश्यक है?
- एक स्वीकारोक्तिपूर्ण एकालाप (सलीलक्वी) का प्रामाणिक मूल्य क्या है?
- क्या स्वीकारोक्ति के साथ-साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करने से अभियुक्त का अपराध सिद्ध होता है?
पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल बड़बड़ाने को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता। अपराधी को किसी और के सामने स्वीकारोक्ति करनी होगी। इसके अलावा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अपर्याप्त थे, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था।
यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त का बड़बड़ाना स्वीकारोक्ति नहीं है, तर्क दिया गया कि स्वीकारोक्ति, चाहे न्यायिक हो या न्यायेतर (एक्स्ट्रा-जुडिशल), के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संवाद की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में स्वीकारोक्ति की अवधारणा के बारे में तर्क दिए और अभियुक्त द्वारा दिए गए आत्म-दोषी (सेल्फ-इन्क्रिमिनेटिंग) बयान की वैधता पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता ने इस मामले में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता और महत्व को चुनौती दी, इसलिए इसकी वैधता का समर्थन करने के लिए पुष्टि करने वाले साक्ष्य की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रतिवादी
इस मामले में, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वैध स्वीकारोक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अधिकारियों के समक्ष ऐसा बयान दिया जाए; उन्होंने तर्क दिया कि केवल बड़बड़ाना ही पर्याप्त है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक श्रृंखला अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है। सुंदरपट्टी द्वारा मदद मांगने के लिए अपने पड़ोसी के घर में भाग जाने की घटना ने अपीलकर्ता और मृतक के बीच दुश्मनी को स्थापित किया। इसके अलावा, कृपा शंकर ने अपीलकर्ता को कुछ बड़बड़ाते हुए घर से निकलते हुए देखा।
इस प्रकार, प्रतिवादियों ने दावा किया कि अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है और वैध साक्ष्य है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्यों के साथ-साथ स्वीकारोक्ति अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने और आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी।

साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) में चर्चित कानून
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से धारा 30 तक के कानून पर चर्चा की गई हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 302
आईपीसी की धारा 302 में “हत्या के लिए सज़ा” का प्रावधान है। जो कोई भी हत्या करता है, उसे मौत या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। हालांकि, धारा 300 में उल्लेख है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, या मृत्यु का कारण बनने का इरादा रखता है या ऐसी शारीरिक चोट कारित करता है जिससे मृत्यु हो सकती है, या यह जानते हुए कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, तो उसे हत्या करना कहा जाता है।’
आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा
इस धारा के तहत, हत्या के लिए “आजीवन कारावास या मृत्यु दंड” का प्रावधान है। न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सज़ा निर्धारित करने का विवेकाधिकार है। यदि हत्या में असाधारण क्रूरता या निर्दयता शामिल है, तो न्यायालय अभियुक्त को मृत्यु दंड दे सकता है।
हत्या और गैर इरादतन हत्या (कल्पेबल होमीसाइड) के बीच अंतर को समझना भी महत्वपूर्ण है। गैर इरादतन हत्या हत्या से ‘छोटा अपराध’ है और इसे आईपीसी की धारा 299 के तहत परिभाषित किया गया है। दोनों के बीच का अंतर “अभियुक्त के इरादे” में निहित है। गैर इरादतन हत्या के मामलों में, अभियुक्त का “मौत पैदा करने का इरादा नहीं रहा होगा, लेकिन उसने असावधान या लापरवाह व्यवहार किया है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की मौत हो गई”। हालाँकि, हत्या के मामले में, अभियुक्त का इरादा व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है।
धारा 302 को ‘गैर-जमानती और गैर-शमनीय (नॉन-कम्पाउंडेबल) योग्य अपराध’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को आसानी से जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है और मामले को शामिल पक्षों के बीच अदालत के बाहर सुलझाया नहीं जा सकता है। अभियुक्त को मुकदमे का सामना करना होगा और अपने कार्यों के पूर्ण परिणामों का सामना करना होगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत ‘स्वीकारोक्ति’
- साक्ष्य अधिनियम के तहत ‘स्वीकारोक्ति’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से धारा 30 स्वीकारोक्ति से संबंधित है। इसके अलावा, यह धारा 164 [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 (जिसे आगे ‘बीएनएसएस’ कहा जाएगा)], 281 (बीएनएसएस की धारा 316) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे “संहिता” कहा जाएगा) की धारा 463 (बीएनएसएस की धारा 511) के तहत प्रदान किया गया है। स्वीकारोक्ति को अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति या अभिस्वीकृति (एकनॉलेजमेंट) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
स्वीकारोक्ति के प्रकार
- न्यायिक स्वीकारोक्ति
न्यायिक स्वीकारोक्ति (जुडिशल कन्फेशन), जैसा कि नाम से पता चलता है, वे स्वीकारोक्ति हैं जो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज की जाती हैं या कानून द्वारा निर्धारित अनुसार अदालत में की जाती हैं। न्यायिक स्वीकारोक्ति का साक्ष्य मूल्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 80 द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि स्वीकारोक्ति मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में या मजिस्ट्रेट द्वारा विधिक कार्यवाही के दौरान दर्ज की गई है, तो ऐसी स्वीकारोक्ति को सत्य और वास्तविक स्वीकारोक्ति माना जाएगा, जिसके आधार पर अभियुक्त पर विधिवत मुकदमा चलाया जा सकता है।
संहिता की धारा 164 मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के स्वीकारोक्तिको दर्ज करने का अधिकार देती है, जिससे यह स्थापित होता है कि स्वीकारोक्ति को दर्ज करना न्यायिक कार्य का एक विशेष क्षेत्र है, तथा कार्यपालिका को स्वीकारोक्ति को दर्ज करने का अधिकार नहीं है।
2. न्यायेतर स्वीकारोक्ति
अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कहीं और किया गया न्यायेतर (एक्स्ट्रा-जुडिशल कन्फेशन) स्वीकारोक्ति या न्यायालय द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को न्यायेतर स्वीकारोक्ति माना जाता है। जब मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान अपराध की स्वतंत्र और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति की जाती है, तो उसे व्यक्ति द्वारा मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में न्यायालय के समक्ष की गई व्यवस्था के आधार पर दोषी याचिका के विरुद्ध न्यायेतर स्वीकारोक्ति कहा जाता है। न्यायेतर स्वीकारोक्ति में न्यायिक स्वीकारोक्ति की तुलना में साक्ष्य संबंधी कम मूल्य होते हैं।
साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता
साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से धारा 30 स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता से संबंधित है।
धारा 24: प्रलोभन, धमकी या वादे द्वारा स्वीकारोक्ति
धारा 24 कुछ स्वीकारोक्ति को अप्रासंगिक मानती है यदि वे किसी प्रोत्साहन, धमकी या वादे के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई हों, विशेषकर जब किसी अधिकारी के समक्ष, न्यायालय की राय में, अभियुक्त व्यक्ति को आधार प्रदान करने के लिए ऐसा किया जाता है,, जो यह मानने के लिए उचित प्रतीत होता है कि ऐसा करने से उसे कोई लाभ मिलेगा या उसके खिलाफ कार्यवाही के बारे में किसी भी अस्थायी प्रकृति की बुराई से बचा जा सकेगा। जो स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से नहीं दी जाती हैं, उन्हें नकली माना जाता है।

ई.डी. स्मिथ बनाम एम्परर (8 नवंबर 1917)
इस मामले में, मद्रास के माउंट रोड में अपना व्यवसाय करने वाले दर्जी श्री ई.डी. स्मिथ, आईपीसी की धारा 411 (बीएनएस, 2023 की धारा 315) के तहत चोरी की संपत्ति के बेईमान कब्जे के लिए मुख्य प्रान्तीय (प्रेसिडेंसी) मजिस्ट्रेट द्वारा सजा के खिलाफ हैं। इस संपत्ति में कई वस्तुएं शामिल हैं, जिनके बारे में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि इन्हें अभियुक्त के परिसर के पास स्थित सेना वस्त्र कारखाने से चुराया गया है। सजा के समर्थन में, मुख्य प्रान्तीय मजिस्ट्रेट ने मुख्य रूप से अभियुक्त द्वारा उस समय दिए गए कुछ बयानों पर भरोसा किया है, जब उसकी दुकान की तलाशी के समय सेना वस्त्र विभाग के अधिकारी ने दूसरे अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच की थी।
यह माना गया कि ये बयान स्वीकारोक्ति हैं और साक्ष्य के रूप में उनकी स्वीकार्यता साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 के तहत वर्जित है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने माना है कि इन धाराओं के अर्थ में कोई स्वीकारोक्ति नहीं है, और आगे बढ़ने से पहले इस साक्ष्य की स्वीकार्यता के प्रश्न का निपटारा करना सुविधाजनक प्रतीत होता है।
धारा 25: पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति को साबित न किया जाना
इस धारा में प्रावधान है कि किसी भी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कोई भी स्वीकारोक्ति साबित नहीं किया जाएगी। यह प्रावधान उन स्थितियों में अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करता है, जहां स्वीकारोक्ति पुलिस हिरासत में प्राप्त की जाती है और उसे जबरन या यातना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर (1939)
पकाला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर मामले में प्रिवी काउंसिल ने फैसला दिया था कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस को दिए गए अभियुक्त के बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के तहत अनुचित रूप से साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 1923 की धारा 34 द्वारा संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया था। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने अपनी राय व्यक्त की कि अभियुक्त का बयान आंशिक रूप से स्वीकारोक्ति और आंशिक रूप से उसकी बेगुनाही का स्पष्टीकरण था। इस विशेष मामले में, यह निर्धारित किया गया कि प्रक्रिया न्याय प्रदान करने में विफल नहीं हुई।
बयान को अस्वीकार किए जाने के बावजूद, अन्य साक्ष्यों से मृतक की अभियुक्त के घर पर उपस्थिति साबित हुई, जो कि बयान का पूरा उद्देश्य था।
धारा 26: पुलिस हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति को उसके विरुद्ध साबित न किया जाना।
धारा 26 में प्रावधान है कि पुलिस हिरासत में ली गया कोई भी स्वीकारोक्ति को किसी व्यक्ति के खिलाफ तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न लिया गया हो। इसके अतिरिक्त, यह धारा यह भी निर्दिष्ट करती है कि “मजिस्ट्रेट” में फोर्ट सेंट जॉर्ज या अन्यत्र प्रान्त में मजिस्ट्रेटी कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले गांव के मुखिया को शामिल नहीं किया गया है, जब तक कि ऐसा मुखिया दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेटी प्राधिकार का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो।

राम नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य (2000)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नरमी बरतने का वादा किए जाने के बाद अभियुक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति धारा 26 के अंतर्गत अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि नरमी का वादा, एक ऐसा वादा था जो अभियुक्त व्यक्ति को यह मानने के लिए उचित आधार देने के लिए पर्याप्त था कि अपराध स्वीकार करने से उसे उचित लाभ मिलेगा।
धारा 27: अभियुक्त से प्राप्त कितनी जानकारी साबित की जा सकती है
यह धारा, धारा 25 और 26 के अपवाद के रूप में कार्य करती है, जहां दोनों धाराएं अभियुक्त को आत्म-दोष लगाने और पुलिस प्राधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करती हैं। धारा 27 में यह प्रावधान है कि, “जब किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से पुलिस अधिकारी की हिरासत में ली गई सूचना के परिणामस्वरूप कोई तथ्य पता चलता है, तो चाहे वह सूचना स्वीकारोक्ति के बराबर हो या न हो, क्योंकि वह सीधे तौर पर उससे प्राप्त तथ्यों से संबंधित है, उसे साबित किया जा सकता है।” दूसरे शब्दों में, इसमें कहा गया है कि यदि अभियुक्त ने पुलिस हिरासत में रहते हुए कोई स्वीकारोक्ति की है, जिससे किसी प्रासंगिक सूचना या तथ्य का पता चलता है, तो ऐसी स्वीकारोक्ति को अदालत में स्वीकार्य माना जाएगा।
मोहन लाल बनाम अजीत सिंह (1978)
मोहन लाल बनाम अजीत सिंह (1978) के मामले में, अभियुक्त ने चोरी की गई वस्तुओं का स्थान बताया, जिसके कारण जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उनकी बरामदगी हुई, और बाद में कुछ दिनों के भीतर ही अभियुक्त द्वारा बताए गए स्थान पर वस्तुएं बरामद कर ली गईं। अदालत ने बयान को महत्वपूर्ण माना और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को हत्या और डकैती का दोषी पाया। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि अभियुक्त के बयान का इस्तेमाल सह-अभियुक्त के खिलाफ नहीं किया जा सकता।
धारा 28: प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण उत्पन्न धारणा को हटाने के बाद की गई स्वीकारोक्ति, प्रासंगिक
धारा 28 प्रलोभन को हटाने के बाद की गई स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता को संबोधित करती है, साथ ही प्रलोभन, धमकी या वादे को हटाने के बाद किए गए स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता को भी संबोधित करती है। यह धारा धारा 24 के तहत दिए गए सामान्य नियम का अपवाद है।
बिहार राज्य बनाम राम बहादुर राय (1958)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व है कि स्वीकारोक्ति किसी भी प्रलोभन को हटाने के बाद स्वेच्छा से की गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकार्यता का परीक्षण यह नहीं है कि प्रलोभन सफल रहा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इसका अभियुक्त पर स्वीकारोक्ति के समय कोई प्रभाव पड़ा था।
धारा 29: अन्यथा प्रासंगिक स्वीकारोक्ति गोपनीयता आदि के वादे के कारण अप्रासंगिक नहीं हो जाएगी
यह धारा यह प्रावधान करती है कि, कोई भी स्वीकारोक्ति जो अन्यथा प्रासंगिक है, गोपनीयता के वादे आदि के कारण अप्रासंगिक नहीं हो जाती। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रासंगिक स्वीकारोक्ति को केवल इस आधार पर बाहर न रखा जाए कि उन्हें कैसे प्राप्त किया गया।
केरल राज्य बनाम राजन (1981)
इस मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने स्वीकारोक्ति के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि “अदालत को मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या स्वीकारोक्ति स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से की गई थी।” न्यायालय ने प्रलोभन और स्वीकारोक्ति के बीच के समय अंतराल, अभियुक्त के आचरण और किसी भी स्वतंत्र पुष्टि की उपस्थिति पर विचार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
धारा 30: सिद्ध स्वीकारोक्ति पर विचार, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा उसी अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचाराधीन अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करती है
यह धारा उन परिस्थितियों में लागू होती है, जहाँ एक ही अपराध के लिए कई व्यक्तियों पर आरोप लगाया जाता है। यह प्रावधान साक्ष्य के रूप में स्वीकारोक्ति के सामान्य नियम से छूट देता है, जिसका उपयोग केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसने उसे बनाया है, अन्य के विरुद्ध नहीं। यह बताता है कि जब एक ही अपराध के लिए कई लोगों पर एक साथ मुकदमा चलाया जाता है, तो किसी एक द्वारा दिया गया स्वीकारोक्ति उन सभी के विरुद्ध स्वीकार्य है।
एम्परर बनाम नन्हू सिंह (1930)
अदालत ने कहा कि एक सह-अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति दूसरे सह-अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसे पुष्टिकारी साक्ष्य के रूप में ध्यान में रखा जा सकता है।

साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) मामले का निर्णय
साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1965) के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अपीलकर्ता साहू को प्रस्तुत साक्ष्यों, जिसमें न्यायेतर स्वीकारोक्ति भी शामिल है, के आधार पर सुदरपट्टी की हत्या का दोषी पाया गया। साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में 16 फरवरी 1965 को, अभियुक्त द्वारा दिया गया मौखिक बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के तहत स्वीकार्य था। अदालत ने आगे कहा कि अभियुक्त द्वारा किसी और के सामने स्वीकारोक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बड़बड़ाना ही पर्याप्त है।
निर्णय के पीछे तर्क
वर्तमान मामले में साक्ष्य की प्रकृति पूरी तरह परिस्थितिजन्य है, सिवाय न्यायेतर स्वीकारोक्ति के। वर्तमान परिस्थितियों को इस नियम पर लागू करने से पहले, न्यायालय ने अभियुक्त की स्वीकारोक्ति की जांच की, जो न्यायेतर थी। न्यायालय ने स्वीकारोक्ति से संबंधित दो मुद्दों की पहचान अलग-अलग रूप में की-
- प्रथम, उस स्थिति में स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता, जहां किसी अन्य के साथ कोई संवाद न हुआ हो; तथा
- दूसरे, ऐसी स्वीकारोक्तियों के प्रामाणिक मूल्य।
तर्क की सामान्य पंक्ति यह है कि स्वीकारोक्ति का अंतर्निहित विचार यह है कि इसे किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है। इसलिए, स्वयं से किया गया स्वीकारोक्ति स्वीकारोक्ति नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से धारा 30 स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता के मुद्दे से निपटती है, लेकिन ‘स्वीकारोक्ति’ शब्द को परिभाषित नहीं करती है। न्यायालय ने पकाला नारायण बनाम आर के मामले का संदर्भ दिया, जिसमें स्वीकारोक्ति को ‘किसी अभियुक्त द्वारा दिए गए एक बयान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें या तो अपराध के संदर्भ में या अपराध का गठन करने वाले सभी तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए।’ हालाँकि, इससे बयान की परिभाषा का सवाल उठा। ‘बयान’ शब्द का शब्दकोश अर्थ है ‘मौखिक रूप से या कागज़ पर बयान करना, सुनाना या पेश करना’। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी दूसरे के साथ संचार स्वीकारोक्ति का एक आवश्यक घटक नहीं है। न्यायालय ने आगे विचार-विमर्श किया कि कानून में ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि किसी दूसरे के साथ संचार को एक आवश्यक घटक माना जाए।
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि किसी स्वीकृति या स्वीकारोक्ति को तब तक स्वीकार किया जा सकता है जब तक वह साबित न हो जाए। उदाहरण एक व्यक्ति A का है, जो व्यक्ति B की हत्या करता है और घटना को किसी अन्य को बताए बिना अपनी डायरी में दर्ज करता है। ऐसे मामले में, अभियुक्त का बयान साबित किया जा सकता है और इसलिए यह उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति मानी जाएगी। मौखिक बयान के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी अन्य को सूचित करना आवश्यक घटक नहीं है।
न्यायालय ने भोगीलाल चुन्नीलाल पंड्या बनाम बॉम्बे राज्य (1958) के मामले का भी उल्लेख किया, इस मामले में मुद्दा यह था कि क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अर्थ में आने वाले गवाह द्वारा दिया गया पूर्व बयान किसी अन्य गवाह की गवाही की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किए जाने से पहले दूसरे को बताया जाना चाहिए। इस मामले में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 157 में प्रयुक्त शब्द ‘बयान’ केवल ‘कुछ ऐसा जो कहा गया है’ को संदर्भित करता है और इसलिए ऐसा बयान जो अपराध स्वीकार करता है, चाहे वह बताया गया हो या नहीं, एक स्वीकारोक्ति के बराबर है। न्यायालय ने माना कि चाहे किसी भी प्रकार की स्वीकारोक्ति हो, यह एक प्रत्यक्ष और प्रासंगिक साक्ष्य है। यह माना जा सकता है कि चूंकि यह बयान देने वाले व्यक्ति के हितों के विरुद्ध है, इसलिए यह सत्य होने की संभावना है। हालांकि, इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले स्पष्ट और तार्किक साक्ष्य का उपयोग करके यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द वास्तव में क्या थे। इसके अलावा, भले ही इस तरह का साक्ष्य साबित हो, लेकिन विवेक और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है और इसे केवल एक पुष्टिकरण साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है। इसलिए, वर्तमान मामले में चूंकि अभियुक्त के शब्दों को सुना गया था और गवाहों का उपयोग करके उसके स्वीकारोक्ति को साबित किया जा सकता था, इसलिए न्यायालय ने इसे पुष्टिकरण मूल्य माना।
न्यायालय ने निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पहचान की-
- अभियुक्त और मृतक के बीच अवैध संबंध;
- जन्माष्टमी के दिन शाम को अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, जब मृतक को उसके पड़ोसी मोहम्मद अब्दुल्ला के बहकावे में आकर अभियुक्त के घर वापस जाने के लिए राजी कर लिया गया था;
- मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था;
- एक महत्वपूर्ण रात के दौरान, 3 व्यक्ति अर्थात् अभियुक्त, मृतक और अभियुक्त का दूसरा बेटा कृपा शंकर घर के अंदर कमरे में सोए थे;
- अगली सुबह जब कृपाशंकर को उसके पिता ने शौच के लिए घर से बाहर जाने को कहा तो तो उन्होंने घर से कुछ गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी और देखा कि उनके पिता अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल रहे थे; तथा
- बाकी गवाहों ने सुबह करीब छह बजे अभियुक्त को घर से निकलते देखा। यह कहते हुए कि उसने सुंदरपट्टी को खत्म कर दिया है और इस तरह उनके दैनिक झगड़े खत्म हो गए हैं।
परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए, न्यायालय केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त ने ही हत्या की होगी, क्योंकि कोई भी उचित वैकल्पिक परिकल्पना प्रस्तुत नहीं की गई थी। यहां, न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के नियम की पुनः पुष्टि की, जो यह है कि यदि परिस्थितियों की श्रृंखला, जिससे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, इतनी पूर्ण है कि वह किसी भी अन्य संभावित परिकल्पना को बाहर कर देती है।

निष्कर्ष
इस लेख के अंत तक, हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकृति और स्वीकारोक्ति, विशेष रूप से स्वीकारोक्ति के बारे में सीखा। स्वीकृति और स्वीकारोक्ति दोनों ही कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से सिविल और आपराधिक मामलों में। हालांकि साक्ष्य अधिनियम में स्वीकृति और स्वीकारोक्ति दोनों को प्रासंगिक टिप्पणियों की आवश्यकता है, उनकी अलग-अलग विशेषताएं और प्रभाव हैं।
स्वीकारोक्ति के विपरीत, स्वीकृति में सिविल कार्यवाही में दिए गए बयान शामिल होते हैं जो या तो उन्हें देने वाले व्यक्ति के पक्ष में या उसके खिलाफ हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वीकारोक्ति विभिन्न परिस्थितियों में की जा सकती है, जिसमें अधिकारियों के साथ मुठभेड़ या पुलिस हिरासत के दौरान भी शामिल है। स्वीकारोक्ति पुख्ता साक्ष्य हो भी सकती है और नहीं भी और इसे संबंधित पक्षों या किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया जा सकता है। इसके विपरीत, आपराधिक मामलों में स्वीकारोक्ति अपराध की प्रत्यक्ष स्वीकृति और अपराध के आसपास की घटनाओं के संबंध में पर्याप्त स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करती है, जो कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, स्वीकारोक्ति न केवल स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति को फंसाती है, बल्कि सह-अभियुक्त पक्षों के लिए भी निहितार्थ रखती है, जो दोषसिद्धि और कानूनी जवाबदेही स्थापित करने में उनके महत्व को रेखांकित करती है। तुलना करने पर वे अधिक साक्ष्य मूल्य रखते हैं, और आम तौर पर अभियुक्त के अपराध का संतोषजनक साक्ष्य माने जाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत स्वीकृति से आप क्या समझते हैं?
स्वीकृति एक ‘बयान है, मौखिक, या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित, जो किसी मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य के बारे में किसी भी अनुमान का सुझाव देता है, और जो किसी भी व्यक्ति द्वारा, और परिस्थिति के तहत किया जाता है।’ स्वीकृति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 17 से 31 में निर्दिष्ट है। धारा 17 से 23 ‘सामान्य स्वीकृति’ को संबोधित करती है, जबकि धारा 24 से 31 ‘स्वीकारोक्ति’ को संबोधित करती है। साक्ष्य में स्वीकृति आत्म-क्षति हो सकती है। धारा 17 स्वीकृति को ‘एक बयान, मौखिक या रिकॉर्ड किया गया, जो प्रश्नगत तथ्य या प्रासंगिक तथ्यों के बारे में किसी निष्कर्ष को इंगित करता है, और जो किसी भी व्यक्ति द्वारा, और इसके द्वारा बताई गई शर्तों के तहत दिया जाता है’ के रूप में परिभाषित करती है।
स्वीकारोक्ति की प्रासंगिकता क्या है?
एक स्वीकारोक्ति उसके निर्माता के खिलाफ साक्ष्य का एक बड़ा टुकड़ा है, और अगर इसे ठीक से दर्ज किया गया है, तो कोई कानूनी समस्या नहीं है। यह उस अभियुक्त की निंदा करने के लिए पर्याप्त होगा जिसने स्वीकार किया है, हालांकि, अदालत को विवेक से बाहर इस पर कार्रवाई करने से पहले पुष्टि की आवश्यकता होती है।
न्यायेतर स्वीकारोक्ति क्या है?
न्यायेतर स्वीकारोक्ति का अर्थ है ‘ऐसा स्वीकारोक्ति जो मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में नहीं की जाती।’ इस प्रकार की स्वीकारोक्ति को साक्ष्य अधिनियम, 1872 में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए साक्ष्य के रूप में इसका महत्व कम है।
संदर्भ