यह लेख Hariharan Y द्वारा लिखा गया है, जो क्राइस्ट (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), बैंगलोर में पढ़ रहे हैं। यह लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 के दंड पहलू से संबंधित है। इस लेख में जिन पहलुओं पर चर्चा की गई है, वे धारा 354, दंड प्रावधानों, राज्य संशोधनों (स्टेट अमेंडमेंट) और संबंधित कानूनी मामलों का अवलोकन (ओवरव्यू) हैं। यह धारा मुख्य रूप से एक महिला की शील (मॉडेस्टी) भंग करने से संबंधित है। अपराध समवर्ती (कन्करेंट) सूची का विषय होने के कारण राज्यों ने सजा के वर्षों की संख्या, अपराध के प्रकार आदि के संबंध में धारा में संशोधन किए हैं। इस लेख का अनुवाद Nisha ने किया है।
Table of Contents
परिचय
महिलाओं के खिलाफ अपराध हमारे समाज में एक सामाजिक बुराई है। आए दिन कोई न कोई महिला के खिलाफ अपराध की खबर सुनने को मिलती है। इस तरह का अपराध बलात्कार, हमला, गंभीर चोट, एसिड अटैक, आपराधिक बल का प्रयोग करके उसकी शील भंग करना आदि हो सकता है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता 1860 में महिलाओं के खिलाफ विशेष अपराधों के प्रावधान हैं और धारा 354 ऐसा ही एक प्रावधान है।
आईपीसी की धारा 354, एक महिला की शील भंग करने से संबंधित है। आईपीसी के तहत ‘शील’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसे मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा पहनावे, आचरण या वाणी में मर्यादा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे व्यवहार के स्त्रीत्व (वोमनली) और विचार, वाणी और अभिव्यक्ति में शुद्धता के रूप में भी देखा जा सकता है। इस प्रकार, शील को एक महिला और उसके व्यवहार में उसके औचित्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह अपराध महिला की शील भंग करने से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायलय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में कहा है कि एक महिला की शील से संबंधित अपराध को मामूली नहीं माना जा सकता है। राजा पांडुरंग बनाम महाराष्ट्र राज्य (2004) में, न्यायालय ने कहा कि एक महिला की शील अनिवार्य रूप से उसका लिंग है और महिला को उसके महिला होने क कारण ज़िम्मेदार ठहराया जाता है इसलिए, धारा 354 एक महिला की शील भंग करने के लिए आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित है। इस खंड को अधिनियमित करने का विधायी (लेजिस्लेटिव) इरादा महिलाओं की सुरक्षा है। इस धारा के तहत किसी पुरुष की शील भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, अदालतों को इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए एक अच्छा संतुलन बनाना पड़ा है। हाल ही में, के. रत्तिया @रत्नाजी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2022) में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर जिस महिला का हाथ पकड़ा जाता है, उसे यह नहीं लगता कि यह उसकी निजता (प्राइवेसी) पर आक्रमण हुआ है, तो यह धारा आकर्षित नहीं होगी।
धारा 354 किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले को दंडित करती है। यह लेख धारा 354 के दंड पहलू और समाज की वर्तमान वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए ऐसी सजा को बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करेगा।
क्या कहती है आईपीसी की धारा 354
धारा 354 में कहा गया है कि जो कोई भी किसी महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का उपयोग करता है या यह जानते हुए कि यह उसकी शील भंग करने की संभावना है, वह इस धारा के तहत सजा का पात्र होगा। सजा या तो विवरण का कारावास है, जो न्यूनतम एक वर्ष होगी और पांच साल तक बढ़ सकती है। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसलिए, न्यायाधीश के विवेक के आधार पर सजा साधारण या कठोर कारावास हो सकती है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के कारावास के साथ जुर्माना लगाया जाएगा, जिसका अर्थ है कि अपराध गैर- समाधेय (कम्पाउंडेबले) है।
धारा 354 की आवश्यक सामग्री
जिस व्यक्ति पर हमला किया गया है वह महिला होनी चाहिए
जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है वह महिला होना चाहिए। हालांकि, दूसरी महिला की शील भंग करने वाली महिला भी इस धारा के तहत दंडनीय होगी।
दृष्टांत: A, एक पुरुष, ने हमला किया और B, एक महिला की शील भंग की। यहां, A को इस खंड के तहत दंडित किया जाएगा यदि वह अन्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है।
दृष्टांत: ‘A, एक महिला, ने हमला किया और ‘B’ एक पुरुष की शील भंग की। यहाँ, A इस धारा के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि B एक पुरुष है। हालाँकि, A पर आईपीसी की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
दृष्टांत: A एक महिला, ने हमला किया और ‘B’, एक महिला की शील भंग की। यहां, A को इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा यदि वह अन्यआवश्यकताओं को संतुष्ट करती है।
आरोपी ने जरूर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया हो
इस धारा के तहत आपराधिक बल का प्रयोग अनिवार्य है। आपराधिक बल को धारा 350 के तहत ऐसे किसी व्यक्ति की सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ जानबूझकर बल का उपयोग करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी भी अपराध के आयोग की ओर जाता है या यह जानते हुए कि वह दूसरे व्यक्ति को चोट, झुंझलाहट (एनॉयंस) या भय का कारण होगा।
उसकी शील भंग करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो
शील के लिए परीक्षण पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1996) के मामले में स्थापित किया गया था। इरादा और ज्ञान इस धारा के दो मुख्य तत्व हैं। हालांकि उन्हें कानून की अदालत में साबित करना मुश्किल है, उन्हें मामले के तथ्यों से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, परीक्षण यह है कि क्या किसी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को इरादा और ज्ञान है कि इससे ऐसी महिला की शील भंग होगी।
इसलिए, धारा 354 के तहत अपराध गठित करने के लिए, उसकी शील भंग करने का इरादा मौजूद होना चाहिए। यह काफी नहीं है कि उसके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया गया है। यह एक उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए कि व्यक्ति की मंशा महिला की शील भंग करने की थी।
राम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1954) में दो लोगों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके कारण एक पुरुष ने एक महिला को धक्का दे दिया। लड़ाई तब से शुरू हुई जब उस पर आरोप लगाया गया कि उसने उसे ‘कामुक (लस्टफुल) आँखों’ से देखा। हालाँकि, इशारे का कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। अदालत ने उसे बरी कर दिया क्योंकि महिला कीशील भंग करने के उसके इरादे का कोई पुख्ता सबूत नहीं था।
एसपी मलिक बनाम उड़ीसा राज्य (1981) में, यह माना गया था कि शील भंग करने के आपराधिक इरादे को साबित किए बिना सार्वजनिक बस में केवल एक महिला के पेट को छूना इस धारा के तहत अपराध के रूप में योग्य नहीं होगा।
आईपीसी की धारा 354 के तहत सजा
इस धारा के तहत निर्धारित सजा के बारे में बहुत बहस और आलोचना हुई है। इससे पहले अधिकतम सजा दो साल कैद और जुर्माना थी। बाद में, 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम ने न्यूनतम एक वर्ष के अधीन, कारावास की सजा को पांच साल के लिया बढ़ा दिया। साथ ही, जुर्माना भी वसूला जाएगा। हालांकि, राज्य के कानूनों के तहत दी जाने वाली सजा में कुछ अंतर हैं जहां राज्यों ने सजा को संशोधित किया है या सजा के स्तर को बढ़ाया है।
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013
पूरे देश को हिला देने वाले निर्भया कांड के मदे नजर देश में आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया था। सरकार ने जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति को कानूनों पर फिर से विचार करने और प्रासंगिक संशोधन करने के लिए बनाया। इस अधिनियम के तहत, सजा को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि तक बढ़ा दिया गया था जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस तरह के सुधार एक जघन्य (हीनियस) सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद किए गए थे। हालांकि, सजा को और बढ़ाने के लिए देश को इस तरह की एक और घटना होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हालाँकि धारा में संशोधन किया गया था, फिर भी हम देखते हैं कि देश में बलात्कार के मामलों की संख्या काफी अधिक है। जब तक विधायिका सजा को और अधिक कठोर नहीं बनाती है, तब तक मामले केवल बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (नेशनल ब्यूरो ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स) ने स्थापित किया है कि महिला के पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता महिलाओं के खिलाफ लगभग तीन प्रतिशत अपराध है।
समिति की सिफारिशें
बलात्कार की सजा
समिति ने सिफारिश की कि बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या कम से कम सात साल के कठोर कारावास की सजा हो। लेकिन, महिला की मृत्यु का कारण या स्थायी (वेजिटेटिव) अवस्था के कारण न्यूनतम बीस वर्ष का कारावास होगा। सामूहिक बलात्कार पर भी यही लागू होगा।
अन्य यौन अपराधों के लिए मान्यता प्राप्त सजा
समिति ने अन्य यौन अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया है। ताक-झांक (वॉयरिज़्म) (सात साल तक की कैद), किसी व्यक्ति का पीछा करना या बार-बार संपर्क करना (तीन साल तक), एसिड अटैक (सात साल तक), और तस्करी (ट्रैफिकिंग) (सात से दस साल तक) की सजा निर्धारित की गई थी।
विवाह का अनिवार्य पंजीकरण
एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि भारत में सभी विवाहों का पंजीकरण एक सक्षम मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में होना चाहिए। यह दहेज मुक्त विवाह सुनिश्चित करने के लिए है।
अन्य सिफारिशें
- बेहतर सुरक्षा, यौन स्वायत्तता (सेक्सुअल ऑटोनोमी) आदि सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के अधिकारों का एक अलग विधेयक (बिल)।
- सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने के लिए सशस्त्र बल विशेष सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा।
- यौन संपर्क के गैर-मर्मज्ञ (पेनेट्रेटिव) रूपों को यौन हमले के रूप में माना जाना।
राज्य सरकारों द्वारा संशोधन
भारतीय दंड संहिता, 1860, उस समय की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के पूर्व तैयार की गई थी। इसलिए, उस समय के विधायकों को लगा कि दो साल की कैद की सजा देना उचित होगा। हालांकि, समय तेजी से बदला है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपराध के आँकड़े केवल ऊपर की ओर रुझान दिखाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक कानूनों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि वे समाज की वर्तमान स्थिति के अनुरूप हैं।
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश इस धारा के तहत, सजा में संशोधन करने और बढ़ाने वाला एकमात्र राज्य था। भारतीय दंड संहिता (आंध्र प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1991 (1991 की अधिनियम संख्या 6) के माध्यम से, सजा को दो साल से बढ़ाकर न्यूनतम पांच साल कर दिया गया, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (2004 के अधिनियम संख्या 14) के माध्यम से धारा 354 में संशोधन किया गया और धारा 354 A नाम से एक नई धारा जोड़ी गई, जिसके तहत निर्धारित सजा कम से कम एक वर्ष की है, जो जुर्माने के साथ दस साल तक बढ़ा दी जा सकती है।
ओडिशा
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहली अनुसूची के तहत, ‘जमानती’ शब्द को ‘गैर-जमानती’ से बदल दिया गया था, जिसका अर्थ है कि उड़ीसा राज्य में अपराध ‘गैर-जमानती’ है।
छत्तीसगढ
छत्तीसगढ़ राज्य ने इस धारा में एक प्रावधान जोड़ा है जिसमें कहा गया है कि अगर शिक्षक, अभिभावक, रिश्तेदार या किसी विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा ऐसा अपमान किया जाता है तो सजा कम से कम दो साल होगी, जिसे जुर्माने के साथ सात साल तक बढ़ाया जा सकता है।
भारत के अन्य राज्यों को भी वर्तमान में निर्धारित सजा को बढ़ाने के प्रावधान में संशोधन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इससे काफी हद तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी।
धारा 354 के तहत सजा का प्रकार
धारा 354 के तहत सजा का कहना है कि यह या तो एक वर्ष से कम नहीं या पांच साल तक का कारावास होगा, और जुर्माना के लिए उत्तरदायी होगा। यहाँ, किसी भी विवरण के कारावास का अर्थ है कि कारावास या तो साधारण कारावास या कठोर कारावास हो सकता है।
भारतीय दंड संहिता दो प्रकार के कारावास का प्रावधान करती है, साधारण कारावास और कठोर कारावास। साधारण कारावास, जैसा कि नाम से पता चलता है, का अर्थ है कि कैदी को कठिन श्रम और अन्य कठोर कार्य नहीं दिए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार बहुत कठोर नहीं होगा। दूसरी ओर कठोर कारावास कैदी को दैनिक आधार पर शारीरिक कार्यों और अन्य प्रकार के श्रम का आवंटन (एलोकेशन) है। ऐसे कारावास आम तौर पर गंभीर अपराधों के लिए दिए जाते हैं, जबकि साधारण कारावास आकस्मिक (कैसुअल) और छोटे अपराधों के लिए दिए जाते हैं।
यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 354 के तहत, न्यायाधीश के पास किसी भी प्रकार का कारावास देने का विवेक है क्योंकि यह ‘दोनों में से किसी भी विवरण का कारावास’ कहता है।
इसके अलावा, इस धारा के तहत सजा का कहना है कि व्यक्ति को कारावास होगा और वह जुर्माना भरने के लिए भी उत्तरदायी होगा। यहाँ ‘और’ शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि कारावास के साथ-साथ व्यक्ति को जुर्माना भी देना होगा। इसलिए, यह एक गैर-समाधेय अपराध है। इसका मतलब यह है कि कारावास अनिवार्य है, और दोषी सिर्फ जुर्माना देकर छूट नहीं सकता है।
इस धारा के तहत जुर्माने की राशि का भी उल्लेख नहीं किया गया है, जो न्यायाधीश को कोई भी जुर्माना लगाने का विवेक देता है जो वह इस धारा के तहत उचित समझे।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रक्रिया
आईपीसी की धारा 354 के तहत एक अपराध एक संज्ञेय (कग्निजेबल) और गैर-जमानती अपराध होगा जो किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
संज्ञेय
एक संज्ञेय अपराध वह है जहां एक पुलिस अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहली अनुसूची या प्रभावी किसी भी अन्य कानून के तहत वारंट के बिना गिरफ्तारी करता है और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकता है। आमतौर पर ऐसे अपराध जिनमें तीन साल से अधिक की सजा होती है, उन्हें संज्ञेय अपराध माना जाता है। एक संज्ञेय अपराध के लिए एक प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है।
गैर जमानती
एक गैर-जमानती अपराध वह है जहां एक अधिकार के रूप में जमानत की मांग नहीं की जा सकती है। अदालत संतुष्ट होने पर जमानत देने का विवेक रखती है।
किसी भी न्यायालय द्वारा विचारणीय
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार किसी महिला की शील भंग करने के अपराध की सुनवाई भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
धारा 354 के तहत मॉडल आरोप
आरोपी के खिलाफ जो मॉडल आरोप तय किया गया है वह इस प्रकार होगा
मैं _______ (पीठा (प्रिसाइडिंग)) अधिकारी का नाम) एतद (हियरबाई) द्वारा आप पर ______ (मामले में अभियुक्त का नाम) निम्नानुसार आरोप लगाता हूं
कि आप थाने _____ जिले के भीतर _______ (स्थान) पर ______ के _______ दिन या उसके आस-पास हैं। कथित ______ ने ______ (पीड़ित का नाम) पर हमला किया (या आपराधिक बल का इस्तेमाल किया), ______ (पीड़ित का नाम) की शील भंग करने के इरादे से (या यह जानते हुए कि यह उसका अपमान करेगा), और इस तरह से भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।
और मैं इसके द्वारा निर्देश देता हूं कि उक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
सबूत का बोझ
आईपीसी के तहत हर आपराधिक अपराध की तरह, इस धारा के तहत आपराधिक मनःस्थिति (मेंस रिया) आवश्यक है। अभियुक्त को अपमान करने का इरादा होना चाहिए या यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके कार्य से महिला की शील भंग होगी। सबूत का भार लोक अभियोजक (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) पर होता है कि वह यह साबित करे कि अभियुक्त का शील भंग करने का इरादा था।
दृष्टांत: ‘A’ ने सीढ़ियाँ चढ़ते समय दूसरी स्त्री को धक्का दे दिया और वह नीचे गिर पड़ी। उसने यह कहते हुए मामला दायर किया कि इससे उसकी शील भंग हुई है। यहां, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है कि वह यह साबित करे कि उसका आपराधिक बल प्रयोग करने या महिला की शील भंग करने के लिए हमला करने का दोषी इरादा था।
धारा 350 के तहत सजा और धारा 354 के तहत सजा में अंतर
धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जिसने किसी व्यक्ति पर जानबूझकर किसी अपराध के आयोग के लिए सहमति के बिना या इस इरादे और ज्ञान के बिना किसी व्यक्ति पर किसी भी बल का इस्तेमाल किया है, तो उसे आपराधिक बल का प्रयोग करना कहेंगे। धारा 350 की सजा धारा 352 के तहत दी जाती है।
धारा 352 में कहा गया है कि जिसने भी गंभीर और अचानक उकसावे के अलावा किसी अन्य तरीके से हमला किया है या आपराधिक बल का इस्तेमाल किया है, वह दोनों में से किसी भी विवरण के कारावास के साथ दंडनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक के जुर्माने के साथ-साथ तीन महीने तक का कारावास हो सकता है।
धारा 350 और धारा 354 के तहत सजा का अंतर
| विवरण | धारा 350 | धारा 354 |
| कारावास की अवधि | दोनों में से किसी भी विवरण के तीन महीने तक | एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन पांच साल तक बढ़ सकती है |
| जुर्माने की राशि | पांच सौ रुपये तक | जुर्माना देय है |
| अपराध की प्रकृति | शमनीय (कम्पाउंडेबले ) | अशमनीय (नॉन कम्पाउंडेबले ) |
धारा 354 और धारा 376 के बीच परस्पर क्रिया (इंटरप्ले)
धारा 354 एक महिला की शील भंग करने से संबंधित है, जबकि धारा 376 बलात्कार के लिए सजा से संबंधित है। अदालतों के पास विभिन्न मामलों में धारा 354 और धारा 376 के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित मामले हैं। दोनों के बीच अंतर की रेखा बहुत बड़ी नहीं है। अदालतों ने मामले की अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर फैसला किया है कि क्या यह शील भंग का अपराध है या बलात्कार; या दोनों है।
धारा 354 और 376 के बीच प्रमुख अंतर अपराध की गंभीरता और सजा की मात्रा है। जबकि धारा 354 के तहत दी जाने वाली अधिकतम सजा पांच साल है, धारा 376 के तहत, सजा न्यूनतम दस साल है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि धारा 376 के तहत अपराध की गंभीरता धारा 354 की तुलना में अधिक गंभीर और जघन्य है।
राम आसरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017) में, आरोपी को अदालत के सामने लाया गया क्योंकि वह एक महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, जिसने उसे मारा और भाग गई। यह माना गया कि उसका यौन संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था, और इसलिए उसे धारा 376 के बजाय धारा 354 के तहत दोषी ठहराया गया।
सजा बढ़ाने की जरूरत है
कड़ी सजा के पक्ष में न्यायिक राय
मध्य प्रदेश राज्य बनाम बबलू (2004)
मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने तत्काल मामले में आरोपी की सजा कम कर दी क्योंकि वह पहला अपराधी था। सर्वोच्च न्यायालय ने, हालांकि, यह माना कि इस तरह की कमी अभियुक्त को अपराध दोहराने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो समाज की नैतिकता के लिए हानिकारक होगा।
इप्पिली त्रिनाधा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1983)
अदालत ने इस मामले में कहा था कि धारा 354 के तहत अपराध के आरोपी अपराधी की परिवीक्षा (प्रोबेशन) केवल असाधारण परिस्थितियों में ही की जा सकती है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के लाभ आरोपी को नहीं दिए गए और इसके बजाय उसे शारीरिक दंड दिया गया। हरीश चंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (1996) के मामले में समान सिद्धांत लागू किए गए थे, जहां अभियुक्तों को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया गया था।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि
भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के साथ, धारा 354 के तहत मौजूदा सजा काफी हद तक अपर्याप्त है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं। इसके अलावा, अदालतों ने लगातार महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान (कॉल्ड) किया है। आंकड़े डरावने हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में महिलाओं के खिलाफ छह मिलियन से अधिक अपराध दर्ज किए गए हैं। 1991 से महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के मामलों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह हर साल ऊपर की ओर रुझान दिखा रहा है, कुछ वर्षों को छोड़कर, जहां इसमें गिरावट का रुख दिखा है। इन अपराधों में बलात्कार, अपहरण, हत्या, जबरन वसूली, घृणा अपराध और एसिड हमले शामिल हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों को उचित सजा दी जाए, यह महत्वपूर्ण है कि अपराधों को रोकने के लिए सख्त और कठोर सजा की आवश्यकता है।
ऐतिहासिक कानूनी मामले
रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल (1995)
मामले के तथ्य
इस मामले को प्रसिद्ध रूप से ‘बट-स्लैपिंग’ मामला कहा जाता है और यह सबसे विवादास्पद मामलों में से एक था। मामले का संक्षिप्त तथ्यात्मक आव्यूह (मैट्रिक्स) यह था कि श्रीमती रूपल देव बजाज पंजाब कैडर से संबंधित एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। जब मामला दर्ज किया गया था, तब वह विशेष सचिव (वित्त) के पद पर कार्यरत थीं। आरोपी ने कथित तौर पर एक बातचीत के दौरान उसके बट पर थप्पड़ मारा था। उसने एक डिनर पार्टी के दौरान पुलिस महानिदेशक (पंजाब) द्वारा आईपीसी की धारा 341, 342, 352, 354 और 509 के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
श्री बजाज, जो एक आईएएस अधिकारी भी हैं, ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जांच में कमी और गिरफ्तारी न होने का आरोप लगाते हुए एक और शिकायत दर्ज कराई। लंबित जांच को पूरा करने के लिए मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट को वापस स्थानांतरित (ट्रांस्फेर्रेड) कर दिया गया था। श्री गिल ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें कथित आधार प्राथमिकी नहीं बनाते थे, आरोप असामान्य थे, और प्राथमिकी दर्ज करने में अनुचित देरी हुई थी। इससे नाराज होकर मिसेज बजाज ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
समस्याएँ
इस मामले में प्रमुख मुद्दे यह थे कि क्या प्राथमिकी में उल्लिखित आरोप आईपीसी के तहत अपराध हैं और क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी को रद्द करना उचित था।
निर्णय
न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966) में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि एक महिला को पीठ पर थप्पड़ मारने का कार्य धारा 354 के तहत उसकी शील भंग करने के योग्य है। श्री गिल का उसके नितंबों (बट्टोक) पर थप्पड़ मारने का ‘दोषपूर्ण इरादा’ (कलपेबेल इंटेंशन) था, जो इस धारा के अंतर्गत आने वाली सामग्रियों में से एक है। हालाँकि, इस मामले में श्री गिल को बरी कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ धारा 341, 342 और 352 के तहत अपराध नहीं बनता था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय का मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को धारा 354 और 509 के तहत दिए गए अपराधों से संबंधित जांच जारी रखने का निर्देश दिया।
निर्णय के बाद
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाया और आरोपी को दोषी ठहराया गया। श्री गिल को धारा 354 के तहत तीन महीने के कारावास और पांच सौ रुपये के जुर्माने और धारा 409 के तहत दो महीने के कारावास और दो सौ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस तरह की सजा के खिलाफ अपील करते हुए, सत्र न्यायालय ने सजा की पुष्टि की लेकिन आरोपी को निर्देश दिया कि वह परिवीक्षा पर रिहा किया लेकिन जुर्माना राशि बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दी गई।
सत्र न्यायालय के फैसले से व्यथित श्री गिल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील की और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दो लाख पच्चीस हजार रुपये और मुकदमेबाजी लागत कर दिया। मामला आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां अपील को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया।
पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह (1966)
मामले के तथ्य
यह मामला इस बात से जुड़ा था कि क्या किसी शिशु को चोट पहुँचाना धारा 354 के तहत एक अपराध के रूप में योग्य होगा। मामले का संक्षिप्त तथ्यात्मक आव्यूह (मैट्रिक्स) यह है कि जब मेजर सिंह ने कमरे में प्रवेश किया, लाइट बंद कर दी, तो बच्चा कमरे में सो रहा था, तब उन्होंने अश्लील हरकत की और बच्चे के निजी अंग में चोट पहुंचाई। कहा जाता है कि जब उसकी मां ने कमरे में प्रवेश किया और लाइट चालू की तो वह भाग निकला।
समस्याएँ
इस मामले में निपटाया गया प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या अभियुक्त धारा 354 के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी है।
निर्णय
न्यायालय ने कहा कि एक महिला, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसमें शील है, जो एक अपमान हो सकता है। ऐसा शील उसे जन्म से ही प्राप्त होता है। अपराध के प्रति महिला की प्रतिक्रिया पर विचार गौण है। इस धारा के तहत एक अपराध को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक सामग्री इरादे और ज्ञान के साथ आपराधिक बल का प्रयोग है, जो दोनों इस मामले में संतुष्ट हो रहे हैं। अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास के साथ एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया, जिसे न देने पर छह माह के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी।
गिरधर गोपाल बनाम राज्य (1952)
तथ्य
याचिकाकर्ता गिरिधर गोपाल को आईपीसी की धारा 342 और 354 के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। साथ-साथ चलने वाले अपराधों के लिए उन्हें छह महीने और एक साल के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। सत्र न्यायाधीश ने सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। इसलिए, याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि धारा 354 के प्रावधान एक व्यक्ति के खिलाफ भेदभावपूर्ण होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं।
मुद्दा
इस मामले में निपटाया गया मुद्दा यह था कि क्या धारा 354, अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की शील भंग करने का प्रावधान नहीं करती है।
निर्णय
न्यायालय ने कहा कि शील भंग करने का कार्य पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी कर सकता है। यहां तक कि एक महिला जो किसी अन्य महिला की शील भंग करती है, वह भी इस धारा के तहत दंडनीय होगी। यह पुरुष या महिला पर समान रूप से कार्य करता है। याचिकाकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति की शील भंग करने का मुद्दा नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि यह वर्ग विधान को प्रतिबंधित करता है लेकिन वर्गीकरण की अनुमति देता है। विधायी मंशा एक महिला की गरिमा और शील की सुरक्षा प्रतीत होती है।
यह तर्क कि यह धारा अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन करती है, भी विफल हो जाती है क्योंकि यह अनुच्छेद केवल जाति, धर्म, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इसलिए, यदि इस तरह का भेदभाव केवल उपरोक्त आधारों पर ही नहीं बल्कि शालीनता, मर्यादा, सार्वजनिक नैतिकता आदि जैसे अतिरिक्त आधारों पर भी है, तो यह मान्य होगा। इसके अलावा, इन कार्यों को अन्य न्यायालयों में भी अपराधीकृत (क्रिमिनिलाइजड) किया जाता है। हर सभ्य देश एक महिला की शील को अपमानित होने से बचाने की कोशिश करेगा। पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।
चैतू लाल बनाम उत्तराखंड राज्य (2019)
तथ्य
आरोपी को आईपीसी की धारा 354, 511 और 376 के तहत दोषी ठहराया गया था। धारा 354 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और धारा 511 व 376 के तहत दोषी ठहराए जाने पर दो वर्ष के अतिरिक्त दो सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। मामले की ओर ले जाने वाले तथ्य यह हैं कि आरोपी ने अपनी चाची से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जो इस मामले में शिकायतकर्ता थी। निचली अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए धारा 354 के तहत एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मुद्दा
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रासंगिक मुद्दा यह था कि क्या एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
निर्णय
अदालत ने निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि धारा 354 के तहत सामग्री को संतुष्ट करने के लिए आपराधिक इरादे और आपराधिक बल का उपयोग होना चाहिए, यह माना जाता है कि वह उचित संदेह से परे दोषी था क्योंकि उसने उसकी शील को ठेस पहुंचाई थी। इसलिए सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। निचली अदालत द्वारा दी गई सजा वैध थी और उसे पहले धारा 354 के तहत एक साल कैद की सजा काटनी होगी जिसके बाद उसे धारा 511 और धारा 376 के तहत दो साल की कैद काटनी होगी।
निष्कर्ष
महिलाओं की सुरक्षा के लिए आईपीसी में धारा 354 एक अहम प्रावधान है। यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक कठोर दंड निर्धारित करने की आवश्यकता है कि अपराध में कमी हो। वर्तमान में, इस धारा के तहत निर्धारित सजा की अधिकतम अवधि पांच वर्ष है। हालांकि, हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह पूरी तरह से अपर्याप्त लगता है। हालांकि, केवल कड़ी सजा से काम नहीं चलेगा। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए कि समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हों।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
धारा 354 को आईपीसी में कब शामिल किया गया था? क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो क्यों?
आईपीसी के लागू होने पर धारा 354 को शामिल किया गया था, यानी 1860 में। 2013 तक निर्धारित सजा अधिकतम दो साल की कैद थी। हालांकि, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए सजा बढ़ाने की जरूरत थी। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया गया, जिसने सजा को अधिकतम दस वर्ष के कारावास तक बढ़ा दिया।
धारा 352 और धारा 354 में क्या अंतर है?
धारा 352 आपराधिक बल से संबंधित है, जबकि धारा 354 विशेष रूप से एक महिला के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हमले या आपराधिक बल से संबंधित है जो उसकी शील भंग करती है।
शील भंग करना बलात्कार से किस प्रकार भिन्न है?
बलात्कार के अपराध की तुलना में एक महिला की शील भंग करने की गंभीरता कम होती है और इसलिए निर्धारित सजा तुलनात्मक रूप से कम होती है।
क्या इस धारा के तहत किसी पुरुष को सुरक्षा उपलब्ध है?
नहीं, केवल एक महिला की शील भंग करना दंडनीय है। हालांकि दूसरी महिला का शील भंग करने वाली महिला भी इस धारा के तहत दंडनीय है।
संदर्भ


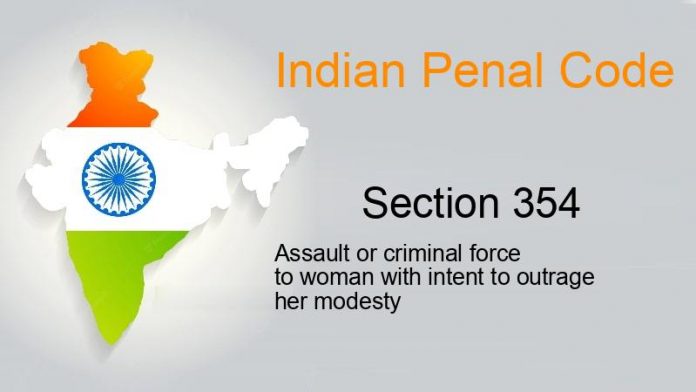
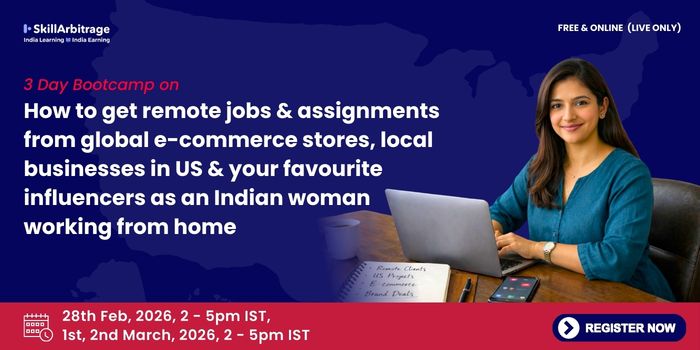







IPC 354 ko sahi dhang se samjhaya gaya hai. thanks