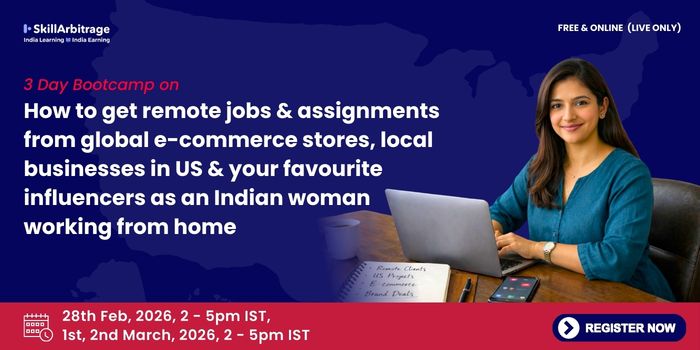इस ब्लॉग पोस्ट में, एनएलयू, ओडिशा से कानून के तृतीय वर्ष के छात्र Vinit Kumar ने “प्राथमिकी (एफआईआर) और पुलिस शिकायत” की अवधारणा (कॉन्सेप्ट) और भारतीय कानूनी व्यवस्था में इसके महत्व का विश्लेषण किया है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
प्राथमिकी दर्ज करने का मूल उद्देश्य आपराधिक कानून को गति देना है न कि उसकी सभी बारीकियों को बताना [1]। प्राथमिकी पुलिस द्वारा दर्ज किए जानेवाले एक आपराधिक मामले का शुरुआती कदम है, और इसमें किए गए अपराध का मूल ज्ञान, अपराध का स्थान, अपराध का समय, पीड़ित कौन था, आदि शामिल होता हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 154 के आधार पर में प्राथमिकी की परिभाषा प्रदान की गई है।, जो बताती है कि:
“एक संज्ञेय (कॉग्नीजेबल) अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी (इनचार्ज ऑफिसर) को मौखिक रूप से दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देशन (डायरेक्शन) में लिखी जाएगी, और जानकारी देनेवाले को पढ़कर बताई जाएगी; और ऐसी हर जानकारी, चाहे लिखित रूप में दी गई हो या ऊपर दिए गए तरीके से जानकारी मिलने पर लिखी गई हो, वह जानकारी देनेवाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, और उसके सार (सब्स्टेंस) को एक पुस्तक में दर्ज किया जाएगा और ऐसे अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए तरीके के अनुसार रखा जाएगा”।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टी.टी.एंटोनी बनाम केरल राज्य और अन्य के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए, सीआरपीसी की धारा 154 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को निर्धारित किया गया है:
“सीआरपीसी की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत दी गई जानकारी को आमतौर पर प्राथमिकी के रूप में जाना जाता है, हालांकि इस शब्द का उपयोग संहिता में नहीं किया गया है … और जैसा कि इसके उपनाम से पता चलता है, यह किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की जानेवाली संज्ञेय अपराध की सबसे पहली सूचना है।”
एक अन्य मामले में, न्यायालय ने कहा कि:
“प्राथमिकी के सभी पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के बाद प्रभारी अधिकारी द्वारा रखी गई एक पुस्तक में एक संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित सूचना के सार को दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल है … जैसा कि सीआरपीसी की धारा 154 में बताया गया है”।
प्राथमिकी कौन दर्ज कर सकता है?
प्राथमिकी एक पीड़ित (विक्टिम), एक गवाह (विटनेस) या अपराध की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है।[6] सीआरपीसी की धारा 154 के तहत निर्धारित कानूनों के अनुसार, शिकायतकर्ता लिखित या मौखिक रूप से अपराध के बारे में जानकारी दे सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकी कौन दर्ज कर सकता है इस संबंध में, यह बताया गया है कि;
“धारा 154 के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विवरण उस व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसे रिपोर्ट की गई घटना की व्यक्तिगत जानकारी हो। यह धारा एक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को दी गई एक संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी की बात करती है।
मौखिक और लिखित रूप में दी गई जानकारी में किसी भी मतभेद की संभावना को रोकने के लिए पुलिस शिकायतकर्ता को मौखिक रूप से बातचीत करने के मामले में प्राथमिकी को वापस पढ़ने के लिए बाध्य (बाइंडिंग) है। इसके अलावा यह शिकायतकर्ता का कर्तव्य है कि अगर उसने टेलीफोन पर सूचना दी है तो वह व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन को आकर उस अपराध के बारे में जानकारी दे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने तेहल सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि:
“यदि एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को टेलीफोनिक संदेश दिया गया है, तो संदेश देने वाला व्यक्ति एक निश्चित व्यक्ति है, या वह व्यक्ति यह पता लगाने में सक्षम है कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दी गई आवश्यक जानकारी को लिखित रूप में लिया गया है और यह इस तरह की जानकारी का विश्वसनीय रिकॉर्ड है और यह जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और उस जानकारी मे कोई भी चीज छुपाई नही गयी है, यह सब जानकारी प्राथमिकी का गठन करती है।
हालांकि एक ऐसे मामले में जहां पुलिस अधिकारी अफवाहें सुनने के बाद घटनास्थल पर गया था, लेकिन उसने पुलिस स्टेशन में एक बयान दर्ज किया, उस समय यह माना गया कि मामले की परिस्थितियों में उस बयान को प्राथमिकी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पुलिस को शिकायतकर्ता को प्राथमिकी की एक कॉपी निःशुल्क देनी होगी।
आरोपी को प्राथमिकी की कॉपी उपलब्ध कराना
भारतीय आपराधिक कानून के तहत, जानकारी देनेवाला, जैसा कि पहले देखा गया है, पुलिस थाने में उसके द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी की एक कॉपी निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है। प्राथमिकी एक आपराधिक मामले में एक आवश्यक दस्तावेज है, जो मुख्य रूप से जानकारी देनेवाले या पीड़ित के मामले का समर्थन कर सकता है। हालाँकि, आरोपी व्यक्ति भी प्राथमिकी की एक कॉपी प्राप्त करने का हकदार है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 आरोपी को प्राथमिकी की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार देती है, ऐसे मामले में जब पुलिस द्वारा जांच पूरी कर ली गई है, और आरोप पत्र (चार्ज शीट) न्यायालय में दायर किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में न्यायाधीश को आरोपी को प्राथमिकी की एक कॉपी निःशुल्क देनी होगी।
इसके अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 (5) और (7) के अनुसार, यह आसानी से निहित किया जा सकता है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पुलिस आरोपी को प्राथमिकी की ‘सी’ कॉपी भी मुफ्त में प्रदान कर सकती है। धारा 207 और 173 की आवश्यक पूर्व-आवश्यकता (प्री रेक्वीजीट) यह है कि पुलिस ने विषयगत मामले में आरोप पत्र दायर किया होगा।
कुछ मामले ऐसे भी हुए हैं जिनमें न्यायालय ने आरोपी को आरोप पत्र दायर करने से पहले और उसके अनुरोध पर और एक निश्चित शुल्क के भुगतान पर भी प्राथमिकी की कॉपी प्रदान की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कि धारा 74 ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ की परिभाषा देता है। कई निर्णयों में, भारत में न्यायालयों ने प्राथमिकी को ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ की परिभाषा में फिट होने के लिए रखा है और इसलिए, यह माना है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के तहत, प्राथमिकी की प्रमाणित (सर्टिफाईड) कॉपी अभियुक्त व्यक्ति के अनुरोध (रिक्वेस्ट) पर प्रत्येक लोक अधिकारी (पब्लिक ऑफिसर) (जैसे पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी) द्वारा ऐसे दस्तावेज की अभिरक्षा (कस्टडी) में लागू कानूनी शुल्क के भुगतान पर दी जानी चाहिए। श्याम लाल बनाम यूपी राज्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय, चन्नप्पा अंडनप्पा सिद्दारेड्डी बनाम राज्य के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला, और मोहम्मद खालिद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय [4 मार्च 2010 को फैसला] इस संबंध में सबसे उद्धृत (साइटेड) फैसले हैं जहां न्यायालय ने माना है कि प्राथमिकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत ‘सार्वजनिक दस्तावेज’ की परिभाषा में फिट बैठती है।
संज्ञेय अपराध (कॉग्निजेबल ऑफेंस)
दिवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(c) के तहत संज्ञेय अपराधों को परिभाषित किया गया है। यह उन अपराधों का वर्ग है जिनमें पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति होती है। ये अपराध प्रकृति में गंभीर हैं, और इस प्रकार इसका उद्देश्य अपराधी या अभियुक्त को दूसरों को नुकसान पहुँचाने से रोकना है। इसलिए, पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है ताकि वारंट जारी करने की सभी कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल कीमती समय की बचत हो सके। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की पहली अनुसूची (शेड्यूल) में संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आने वाले अपराधों को निर्दिष्ट किया गया है। हालांकि संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों में अपराधों के वर्गीकरण का कोई पूर्व-निर्धारित पैटर्न नहीं है लेकिन एक अध्ययन पर यह देखा जा सकता है कि तीन वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों को संज्ञेय अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और जिनकी सजा तीन साल से कम है उन्हें असंज्ञेय अपराधों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
धारा 156(1) के अनुसार, पुलिस को न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना एक संज्ञेय अपराध से जुड़े मामले की जांच करने का अधिकार है। धारा 156(1) बताती है कि:
“पुलिस थाने का कोई भी प्रभारी अधिकारी, न्यायाधीश के आदेश के बिना, किसी भी संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जो कि ऐसे थाने की सीमा के भीतर स्थानीय क्षेत्र (लोकल एरिया) पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालय के पास जांच करने या अध्याय XIII के प्रावधानों के तहत प्रयास करने की शक्ति होगी।”
धारा 156 (2) आगे पढ़ते है,
“ऐसे किसी भी मामले में किसी पुलिस अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को किसी भी स्तर पर इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसकी जांच करने के लिए इस धारा के तहत उस अधिकारी को अधिकार नहीं दिया गया था।”
शब्द ‘संज्ञान’ (कॉग्नीजेंस) को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। आपराधिक कानून या प्रक्रिया में इस शब्द का कोई गूढ़ या रहस्यमय महत्व नहीं है। न्यायालयों या न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में, इसका सामान्य अर्थ है जब न्यायालय ‘न्यायिक रूप से नोटिस लेता है।’
एक प्राथमिकी और एक पुलिस शिकायत के बीच अंतर
प्राथमिकी और पुलिस शिकायत के बीच अंतर का मुख्य बिंदु यह है कि एक प्राथमिकी एक संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है जबकि एक पुलिस शिकायत गैर-संज्ञेय और संज्ञेय दोनों प्रकार के अपराधों के लिए दर्ज की जा सकती है। यद्यपि दोनों का मूल अर्थ एक शिकायत है, लेकिन वे उन अपराधों के संदर्भ में भिन्न हैं जिनसे वे निपटते हैं, दंड, कानूनी परिणाम, साक्ष्य मूल्य, आदि। एक न्यायाधीश को एक शिकायत मौखिक शब्दों के माध्यम से दी जाती है या लिखित रूप में, जबकि प्राथमिकी अपराध करने के स्थान के पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(d), एक शिकायत के तथ्य का किया जानेवाला आरोप है जो एक शिकायत का गठन करता है। इसके अलावा, एक शिकायतकर्ता और प्रथम मुखबिर (इनफॉरमेंट) का एक ही व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है। भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता इसके लिए कोई सख्त रूप प्रदान नहीं करती हैं, और इस प्रकार एक हलफनामा या एक याचिका भी न्यायालय में एक शिकायत कही जा सकती है। सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध के घटित होने की जानकारी है, वह शिकायत दर्ज करा सकता है, भले ही संबंधित व्यक्ति अपराध से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित न हुआ हो, लेकिन इसमें विवाह से संबंधित अपराध, मानहानि (डीफमेशन) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 से 197 में वर्णित अपराध शामिल नहीं होते। जब कोई जानकारी देनेवाला किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना के संबंध में पुलिस अधिकारियों से संपर्क करता है तो इसे शिकायत दर्ज करना कहा जाता है। यह ‘पहली सूचना’ एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है, जैसा कि मुखबिर द्वारा बताया जाती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154, यह प्राथमिकी’ का गठन करती है और बाद की घटनाओं के आलोक में इस धारा के अर्थ के भीतर दी जानेवाली जानकारी का खुलासा करती है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 190 के तहत एक न्यायाधीश धारा 200 के तहत तथ्यों और गवाहों की जांच करके एक शिकायत का संज्ञान ले सकता है। यदि वह पाता है कि शिकायत योग्यता (मेरिट्स) के साथ है, तो मामले को परीक्षण (ट्रायल) के लिए सही माना जाता है और न्यायाधीश धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करता है। यदि अपराध विशेष रूप से सत्र (सेशन) न्यायालय द्वारा विचारणीय (ट्रायबल) है, तो न्यायाधीश मामले को धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय में भेज देता है।
धारा 190 के अनुसार, न्यायाधीश को उसमें दिए गए तीन तरीकों से अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है। हालांकि, अगर वह एक शिकायत के आधार पर संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है तो मामले की जांच और निर्णय लेने के लिए, वह अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 से 203 द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है और यदि मामले के तथ्यानुसार आवश्यक हो, तो धारा 204 के तहत भी।
यदि प्राथमिकी के मामले में शामिल अपराध संज्ञेय प्रकृति का होता है तो ऐसे मामले में पुलिस को न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उक्त मामले में जांच शुरू करने और फिर आरोप पत्र दायर करने का अधिकार है। दूसरी ओर, जब एक न्यायाधीश किसी शिकायत के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेता है, तो वह मामले की जांच का आदेश देता है और अगर उसे लगता है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, तो वह पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दे सकता है। उसे शिकायत पर स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा कोई गंभीर अपराध नहीं है जिसके लिए उन्हें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। वह शिकायत पर तभी कार्रवाई कर सकता है जब उससे प्रथम दृष्टया (प्रीमा फेसी) किसी अपराध के होने का पता चलता है।
न्यायालय ने पी. कुन्हुमुहम्मद बनाम केरल राज्य के मामले में कहा कि:
“धारा 155(2)[3] के विपरीत जांच के बाद एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को धारा 2(d) और धारा 190(1)(a) के तहत शिकायत माना जा सकता है, अगर जांच शुरू होने पर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि मामला एक संज्ञेय अपराध के घटित होने में शामिल है या यदि इसके बारे में कोई संदेह है और जांच केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में बताती है”।
इस प्रकार, यदि जांच के प्रारंभिक चरणों में, यह पाया जाता है कि किया गया अपराध गैर-संज्ञेय प्रकृति का है, तो जांच के बाद प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (d) या धारा 190(1)(a) के दायरे में ‘शिकायत’ के रूप में नहीं माना जा सकता है।
प्राथमिकी के मामले में, पुलिस को मामले की जांच करने और उसके बाद मिलने वाले सबूतों की तलाशी लेने और उन्हें जब्त करने का अधिकार है। पुलिस तब जांच के अंत में आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद, न्यायालय आरोपों पर फैसला करता है।
जब एक प्रभारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर किए गए अपराध के संदर्भ में खुलासा एक जानकारी देनेवाले व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है, और प्रभारी पुलिस को पता चलता है कि वह एक गैर-संज्ञेय अपराध है। ऐसे समय जानकारी मिलने पर उस पुलिस को स्टेशन डायरी में मामले की जानकारी दर्ज करनी होती है और सूचना देने वाले को संबंधित न्यायाधीश से संपर्क करने के लिए संदर्भित करना होता है। जिनके आदेश पर पुलिस ऐसे मामलों की जांच उन्हीं शक्तियों के साथ कर सकती है जो एक संज्ञेय मामले में होती हैं, सिवाए बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति भी इस्तेमाल की जा सकती है। जहां कोई मामला दो या दो से अधिक अपराधों से संबंधित है, जिनमें से एक संज्ञेय है, तो मामले को एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा, इस तथ्य के बावजूद कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं।
पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार करना
कभी-कभी, पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर सकती है। यह कानूनी और गैर कानूनी दोनों हो सकता है। ऐसे मामलों में जहां उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है या संज्ञान लेने की उनकी कानूनी क्षमता नहीं है या अपराध गैर-संज्ञेय प्रकृति का है, इसे कानूनी माना जाएगा। लेकिन जहां पुलिस ठोस कानूनी आधार के बिना स्पष्ट कारणों से शिकायत दर्ज करने से इनकार करती है, यह कानून के विपरीत है। जब एक पुलिस अधिकारी इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करता है कि यह एक गैर-संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है, तो उसे जानकारी देनेवाले को सूचित करना चाहिए और उसे न्यायाधीश को शिकायत दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए। यदि किया गया अपराध किसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो सूचना दर्ज की जानी चाहिए और अधिकार क्षेत्र वाले उपयुक्त पुलिस स्टेशन को अग्रेषित (डायरेक्ट) की जानी चाहिए, अन्यथा इस आधार पर रिकॉर्ड करने से इनकार करना कर्तव्य की अवहेलना होगी।
किसी भी जानकारी को दर्ज करने की अनिवार्यता भी इस समझ पर आधारित है कि प्राथमिकी कोई ठोस सबूत नहीं है, और इसका उपयोग केवल जानकारी का खंडन या पुष्टि (कॉन्ट्रेडिक्ट एंड कॉरोबोरेट) करने के लिए किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 155(1) के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी को पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में किए गए गैर-संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलने पर, उसे स्टेशन डायरी में मामले की जानकारी दर्ज करनी चाहिए और जानकारी देने वाले को संबंधित न्यायाधीश से संपर्क करने के लिए संदर्भित करना चाहिए।
उपचार
- यदि संबंधित अधिकारी धारा 154(3) के तहत अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एक संज्ञेय अपराध के आयोग के बारे में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करता है, तो ऐसे समय जानकारी देनेवाला लिखित शिकायत के साथ पुलिस अधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) या पुलिस आयुक्त (कमिशनर) के पास जा सकता है। यदि, शिकायत के विश्लेषण पर, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त संतुष्ट होते हैं कि यह एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है, तो वह या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या अपने अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) को प्राथमिकी दर्ज करने और मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दे सकता है।
- यदि ऊपर बताए गए उपाय व्यर्थ जाते हैं, तो जानकारी देने वाला कानूनी रूप से धारा 156(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट/मेट्रोपॉलिटन न्यायाधीश के पास आपराधिक प्रक्रिया की धारा 190 के तहत शिकायत दर्ज करने का हकदार है, जिससे प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर मामले की जांच किए जाने की प्रार्थना की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ अपने कार्य से चूक करनेवाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध परमादेश (मैंडमस) जारी करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जा सकती है, ताकि प्राथमिकी दर्ज की जा सके और उसे कारण बताने का निर्देश दिया जा सके, जैसे की:
- उसने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की;
- ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए उनके खिलाफ “कदाचार” (मिसकंडक्ट) के लिए अनुशासनात्मक (डिसिप्लिनरी) कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए;
- न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और आरोपी व्यक्ति को बचाने के लिए उसे पुलिस सेवा से निलंबित (सस्पेंड) क्यों नहीं किया जाना चाहिए। एक दीवानी मामले में, उस अधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका (कंटेंप्ट पिटीशन) दायर की जा सकती है जिसने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ललिता कुमारी मामले में यह माना है कि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए जहां शिकायत एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।
- क्षेत्राधिकार के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने पर अब एक पुलिसकर्मी को एक साल की जेल हो सकती है। एक पत्र याचिका दायर की जा सकती है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जा सकती है, और उनसे न्यायालय की कथित अवमानना के लिए सुओ मोटो संज्ञान लेने की प्रार्थना की जा सकती है। इसके अलावा, उक्त पत्र की एक प्रति संबंधित पुलिस अधिकारी को भेजी जा सकती है। ऐसी पत्र याचिका की स्थिति सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत एक आवेदन (एप्लीकेशन) के माध्यम से पूछी जा सकती है।
- यदि शिकायत/प्राथमिकी दर्ज न करने पर पुलिस की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को “जीवन और स्वतंत्रता” से हताशा/वंचित होना पड़ता है, तो हर्जाना/मुआवजे (कंपनसेशन) की मांग के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।
- इसके अलावा, धारा 166A(c) के तहत, यदि संबंधित लोक सेवक आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उप-धारा (1) के तहत उसे दी गई किसी भी जानकारी को दर्ज करने में विफल रहता है, तो धारा के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में धारा 326A, धारा 326B, धारा 354, धारा 354B, धारा 370, धारा 370A, धारा 376, धारा 376A, धारा 376B, धारा 376C, धारा 376D, धारा 376E या भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के तहत वह कठोर कारावास से दंडनीय है। जिसकी अवधि छह महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जो दो साल तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सूचना की वास्तविकता, और विश्वसनीयता सूचना दर्ज करने से इंकार करने का कोई आधार नहीं है। एक अन्य मामले में, यह माना गया कि सूचना दर्ज करने से इंकार करना एक लोक अधिकारी द्वारा कर्तव्य की घोषणा (डिक्लेरेशन) है। हालांकि, शिकायत दर्ज करने से इनकार करने के लिए प्रदान किए गए उपचारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, न्यायालय ने फैसला दिया है कि:
“सूचना का एक अस्पष्ट, अनिश्चित या अनधिकृत टुकड़ा केवल पहली सूचना के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह पहली बार प्राप्त हुआ था। इसी तरह फोन पर एक अस्पष्ट संदेश केवल यह कहते हुए कि एक व्यक्ति सड़क पर मृत पड़ा है, प्राथमिकी नहीं बनता है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के तहत विधायिका (लेजिस्लेचर) द्वारा ‘सूचना’ शब्द का सावधानीपूर्वक उपयोग किया गया है। “जिसमें अभिव्यक्ति,” उचित शिकायत” और “विश्वसनीय जानकारी” का उपयोग किया जाता है। जाहिर है, संहिता की धारा 41(1)(a) और (g) के विपरीत धारा 154(1) में “सूचना” शब्द की गैर-योग्यता इस कारण से हो सकती है कि पुलिस अधिकारी को एक संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित जानकारी और उस पर इस आधार पर मामला दर्ज करने के लिए एक रिकॉर्ड करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि वह सूचना की तर्कसंगतता या विश्वसनीयता से संतुष्ट नहीं है।”
काथिरावन बनाम राज्य में, न्यायालय ने कहा कि:
“यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाली शिकायत (सूचना) प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी मामला दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं और ऐसे अधिकारी यह पता लगाने के लिए आरोपों की जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या मामला दर्ज करने से पहले वे सही हैं या नहीं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी मामले में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी यह निर्णय लेने के लिए प्रारंभिक जांच नहीं कर सकते हैं कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार जांच के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। लेकिन ऐसे मामले सामान्य नियम के अपवाद मात्र हैं। इस तरह के अपवाद को पुलिस द्वारा यह कहने के लिए सामान्यीकृत (नॉर्मलाइज) नहीं किया जाना चाहिए कि पुलिस के पास मामला दर्ज करने या न करने, प्रारंभिक जांच करने या वह एक अपराध ही की नही का निर्णय लेने का विवेक (डेस्क्रिशन) है।
साक्ष्य मूल्य
पुलिस तीन तरह के बयान दे सकती है। पहली तरह का बयान वह है जिसे प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया जा सकता है, दूसरे तरह का बयान वह है जिसे जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किया जा सकता है, और तीसरे तरह का बयान किसी भी तरह का बयान है जो ऊपर उल्लिखित दो श्रेणियों में से किसी के भी अंतर्गत नहीं आता है।
साक्ष्य विशेष सटीकता या परिस्थितियों पर तथ्यों को प्रकट करने वाली गवाही का मामला है।
प्राथमिकी को न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सबूत नहीं माना जाता है क्योंकि यह मुकदमे के दरमियान नहीं दी जाती है, और यह शपथ के अभाव में दी जाती है, और जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) द्वारा इसकी जांच नहीं की जाती है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए किसी भी अन्य बयान की तुलना में प्राथमिकी का महत्व कहीं अधिक है। यह पुलिस को किसी अपराध के घटित होने के बारे में प्राप्त होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है और इस प्रकार इसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 के तहत जानकारी देनेवाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कहानी की पुष्टि करने या न्यायालय द्वारा मामले में गवाह के रूप में बुलाए जाने के मामले में अधिनियम की धारा 145 तहत तथ्यों के अपने संस्करण (वर्जन) का खंडन (कॉन्ट्रेडिक्ट) करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के विश्लेषण पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि परिस्थितियाँ किसी भी प्रकार के गवाह की गवाही की पुष्टि की मांग करती हैं, तो धारा 157 को लागू करना होता है जो यह बताती है कि किसी भी रूप की पुष्टि के लिए पहले के बयान को उसी तथ्य या उसी समय से संबंधित होना चाहिए, यह एक प्राधिकरण (अथॉरिटी) के समक्ष भी होना चाहिए जिसके पास जिसके बारे में चर्चा की जा रही है ऐसे विशेष तथ्य की जांच करने की कानूनी क्षमता हो, और न्यायालय में इसे साबित करने की जरूरत होती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने निसार अली बनाम यूपी राज्य के मामले में अलग राय देते हुए कहा है कि:
“प्राथमिकी एक प्रकार का साक्ष्य है जिसका विरोधाभासी मूल्य (कॉन्ट्रेडिक्टरी वैल्यू) केवल उस व्यक्ति के लिए है जिसने प्राथमिकी दर्ज की है (जानकारी देनेवाला व्यक्ति) और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति, गवाह द्वारा दिए गए बयान का खंडन करने के लिए नहीं किया जा सकता है”।
दामोदर प्रसाद बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिया गया निर्णय न्यायालय के इस दृष्टिकोण को और मजबूत करता है, जो कहता है:
“यह आवश्यक रूप से वह व्यक्ति होना चाहिए जो पहली बार में अपराध के बारे में पुलिस को सूचित कर रहा हो।”
आरोपी प्राथमिकी दर्ज करने वाले व्यक्ति को कम विश्वसनीय दिखाने के लिए प्राथमिकी का उपयोग कर सकता है और इसलिए सबूत के एक भाग के रूप में प्राथमिकी का मूल्य कम हो जाता है। हालाँकि यह केवल जानकारी देनेवाले पर लागू होता है और किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। भले ही जानकारी देनेवाले व्यक्ति द्वारा जानकारी खंडित की गई हो और प्राथमिकी कुछ विश्वसनीयता खो देती है, ऐसे समय अन्य गवाह आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं, यानी प्राथमिकी का मूल्य इतना पर्याप्त नहीं है।
ऐसा हो सकता है कि जानकारी देनेवाला व्यक्ति खुद ही आरोपी हो। ऐसे मामलों में, उसके द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह हमारे संविधान की बुनियादी संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) में सन्निहित (ऐम्बोडिड) है कि किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कई मामलों में, न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि प्राथमिकी के आधार पर एकमात्र संभावित कार्रवाई साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे जानकारी देनेवाले व्यक्ति द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि या खंडन करना है। न्यायालय ने आगे कहा कि अगर बतानेवाला/करनेवाला भी आरोपी है तो ऐसे समय भी यह संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:
“प्राथमिकी की जानकारी का उपयोग केवल कार्य करनेवाले के विरोधाभास और पुष्टि (कॉन्ट्रेडिक्शन एंड कॉरोबोरेशन) के लिए किया जा सकता है और किसी अन्य चश्मदीद गवाह के लिए नहीं।”
यह पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य में यह बताया गया था, कि यह काफी अच्छी तरह से स्थापित है कि प्राथमिकी सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा नहीं है और इसका उपयोग केवल उस जानकारी देनेवाले की गवाही को खराब (डिसक्रेडिट) करने के लिए किया जा सकता है और इसका उपयोग अन्य गवाहों की गवाही का खंडन करने या उसे बदनाम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
इकबालिया बयान (कन्फेशनल स्टेटमेंट)
जहां प्राथमिकी में बताए गए व्यक्ति को समन किया जाना है, और अगर आरोप पत्र तैयार नहीं की गई है तो प्राथमिकी का सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह उस स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत है। इसके अलावा, यदि प्राथमिकी इकबालिया है, तो यह स्वीकार्य हो सकती है। एक स्वीकारोक्ति (कन्फेशन) इस अनुमान पर साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा बयान नहीं देगा जो उसके या उसके हित के खिलाफ हो, जब तक कि यह सच न हो। अभियुक्त (एक्यूज्ड) द्वारा स्वीकारोक्ति के मामले में, न्यायालय को दो परीक्षणों पर गौर करना चाहिए, अर्थात (a) क्या स्वीकारोक्ति पूरी तरह से स्वैच्छिक (वॉलिंटरी) है, और (b) यदि ऐसा है, तो क्या यह सच और भरोसेमंद है। पहले परीक्षण की संतुष्टि साक्ष्य में इसकी स्वीकार्यता के लिए अत्यावश्यक है और यदि मामले की परिस्थितियां इसकी स्वैच्छिक प्रकृति पर कोई संदेह पैदा करती हैं तो स्वीकारोक्ति को हमेशा खारिज कर दिया जाना चाहिए। यदि स्वीकारोक्ति को प्रलोभन (इंड्यूसमेंट), धमकी या वादे के परिणामस्वरूप दिखाया गया है, तो यह साक्ष्य में अस्वीकार्य है क्योंकि इसमें अभियुक्त की ओर से स्वैच्छिक कार्रवाई के महत्वपूर्ण तत्व का अभाव होगा और यह अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, धमकी, ब्लैकमेलिंग आदि का परिणाम हो सकता है।
जहां तक दूसरे परीक्षण की बात है, न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्य, इस प्रकार दिए गए बयान की जानकारी की जांच करनी चाहिए और फिर उन पर संभाव्यता (प्रोबेबिलिटी) का परीक्षण लागू करना चाहिए। अगर न्यायालय को पता चलता है कि इकबालिया बयान में दिया गया तात्विक (मटेरियल) बयान चश्मदीद गवाह के साक्ष्य के साथ असंगत है, तो यह माना जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि इकबालिया बयान सच है और इसे अलग रखा जाना चाहिए।
स्वीकारोक्ति इसके निर्माता के खिलाफ इस शर्त पर दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकती है कि यह सत्य और स्वैच्छिक है; यह उस विशेष मामले की परिस्थितियों में फिट बैठता है जो कम से कम यह धारणा बना सकता है कि यह सच है और यह या तो अपराध के संदर्भ में या कम से कम उन सभी तथ्यों को स्वीकार करता है जो अपराध का गठन करते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि एक सच्चे और स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति को उस जानकारी देनेवाले के खिलाफ उपयोग करने के लिए भौतिक रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि “हालांकि प्राथमिकी को अपराध से संबंधित कारकों (फैक्टर्स) के एक विश्वकोश के रूप में नहीं माना जाता है, फिर भी अपराध के संबंध में कुछ निश्चित जानकारी होनी चाहिए”।
मुखबिर की मौत
कुछ मामलों में, प्राथमिकी का उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) या अधिनियम के धारा 8 के तहत जानकारी देनेवाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण या उसके आचरण के एक भाग के रूप में किया जा सकता है। यदि जानकारी देनेवाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो प्राथमिकी को निर्विवाद रूप से एक ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राथमिकी को एक ठोस सबूत के रूप में लेने से पहले एक पूर्व-अपेक्षित (प्री-रिक्विजिट) शर्त पूरी करनी होगी यानी जानकारी देनेवाले व्यक्ति की मौत का प्राथमिकी से संबंध होना चाहिए या दायर की गई प्राथमिकी के संबंध में किसी सबूत के साथ कुछ लिंक होना चाहिए, यह विचार दामोदर प्रसाद बनाम यूपी राज्य के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के तहत न्यायालय द्वारा की गई है और यह न्यायालय द्वारा पहले कपूर सिंह बनाम एंपरर के मामले में प्रदर्शित किया गया था। इस भूमि की न्यायालयों ने यह भी कहा है कि अगर प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद जानकारी देनेवाला व्यक्ति अपनी चोटों से मर जाता है, तो प्राथमिकी मृत्युकालिक बयान (डाईंग डिक्लेरेशन) हो सकती है। हालांकि, जब प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को फंसाया जाता है जो आरोपी है और इसमें घटना का विवरण शामिल है, तो इसे मरने से पहले दिया गया बयान नहीं माना जाता है। दी गई जानकारी में निश्चितता का आवश्यक तत्व पूरा होना चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वह जानकारी गायब हो सकती है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्राथमिकी एक मृत व्यक्ति द्वारा एक पर्याप्त रूप में माना जाता है, इसकी जानकारी/विवरण को साबित किया जाना चाहिए। “इसकी पुष्टि की जानी चाहिए और यह साबित किया जाना चाहिए कि संबंधित मामले में इसका कोई मूल्य है।” इस दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, आगे यह अभिनिर्धारित (कंसोलिडेट) किया गया कि:
“यदि मुकदमे के दौरान प्राथमिकी दायर करते वक्त जानकारी देनेवाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और अभियोजन पक्ष प्राथमिकी को उसकी मृत्यु के सवालों का पता लगाए बिना मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में मानना शुरू कर देता है, तो यह मरने से पहले का बयान नहीं हो सकता है”।
प्राथमिकी का उपयोग बचाव पक्ष द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-155(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने वाले व्यक्ति की साख (क्रेडिट) पर महाभियोग (इंपीच) लगाने के लिए किया जा सकता है।
यदि मुखबिर की मृत्यु का दर्ज की गई शिकायत से कोई संबंध नहीं है, अर्थात उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है और किसी मामले के संबंध में उसे लगी चोटों के कारण दम नहीं तोड़ता है, तो शिकायत लागू नहीं होती है। न्यायालय ने उमराव बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इस दृष्टिकोण को सही ठहराया है, यह फैसला देते हुए कि:
“शिकायतकर्ता, जिसे बेरहमी से पीटा गया था, अगर उसकी मौत प्राकृतिक रूप से होती है न कि उसे लगी चोटों के कारण, तो ऐसे वक्त धारा 32 (1) लागू नहीं होगी”।
सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के किसी भी दुरुपयोग को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह माना है कि:
“शिकायतकर्ता की मृत्यु के कारण उसकी जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले में अपने आप में तथ्यात्मक नहीं हो सकता है, और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय में गवाहों द्वारा प्रकट की गई अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) कहानी प्राथमिकी की जानकारी के विपरीत है, तो इसका एक प्रभाव हो सकता है और दूसरी ओर, यदि प्राथमिकी की जानकारी परीक्षण के दौरान साक्ष्य के अनुरूप है, तो इसका पूरी तरह से एक अलग प्रभाव जो सकता है।”
प्राथमिकी का मूल्य प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सूचना, और अपराध को देखने के तरीके पर निर्भर करता है। पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु पूर्व कथन के रूप में लिया गया है, जब व्यक्ति मृत्यु पूर्व बयान दर्ज कराने के लिए जीवित नहीं रहा।
प्राथमिकी दर्ज करने में देरी
कानून के अनुसार, प्राथमिकी जल्द से जल्द दर्ज की जानी चाहिए ताकि समय बर्बाद न हो और अपराधी को समय पर पकड़ा जा सके और दूसरों को कोई खतरा न हो। लेकिन कई बार प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हो जाती है। यह अज्ञानता या पुलिस की कार्रवाई या प्राथमिकी की जानकारी देनेवाले द्वारा स्वयं की गलती के कारण हो सकता है। यदि पुलिस की ओर से देरी होती है, तो उन्हें इस तरह की देरी के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करना चाहिए और देरी का कोई अस्पष्ट आधार कानून की नजर में पर्याप्त नहीं होगा। यदि देरी अपरिहार्य (इनएविटेबल) और उचित आधार पर हुई तो पुलिस भारतीय आपराधिक कानून के तहत उत्तरदायी नहीं होगी। इसके अलावा, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के ऐसे विभिन्न संदर्भों के अलग-अलग कानूनी परिणाम होते हैं। हालांकि कानून ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया है, यह एक स्वीकृत नियम है कि इसे तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए। यदि देरी हुई है तो देरी के लिए स्पष्टीकरण प्राथमिकी में दिया जाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की देरी अलंकरण (एंबेलिशमेंट) का कारण बन सकती है, जिसे न्यायालय में बाद का विचार माना जा सकता है। बथुला नागमल्लेश्वर राव और अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि द्वारा लोक अभियोजक में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
“प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, अगर उचित रूप से समझाई जाए, तो घातक नहीं होगी। प्राथमिकी दर्ज करने में अनुचित देरी को हमेशा एक निश्चित मात्रा में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और जहाँ तक संभव हो इससे बचा जाना चाहिए।”
प्राथमिकी में देरी निम्नलिखित तीन श्रेणियों के तहत समझी जा सकती है:
- प्राथमिकी के लिए जानकारी देनेवाले व्यक्ति द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी।
- पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी ।
- न्यायाधीश को प्राथमिकी भेजने में देरी।
मुखबिर द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब
प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी पर निर्णय लेते समय न्यायालय विभिन्न छोटे मोटे बिंदुओं पर विचार कर सकता है, जैसे कि निकटतम पुलिस थाने और अपराध के स्थान के बीच की दूरी, अपराध करने का समय, क्या प्राथमिकी की जानकारी देनेवाले के पास कोई वाहन था जब उसने पुलिस से संपर्क किया था, अपराध का प्रकार, पीड़ित पक्ष की सामाजिक और वित्तीय स्थिति, उनका क्षेत्र, आदि। न्यायालय ने मुन्ना @ पूरन यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में कहा कि गाँव और थाने के बीच की छह किलोमीटर की दूरी को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता और इस दूरी के परिणामस्वरूप प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग एक घंटे की देरी हुई और इसलिए उस प्राथमिकी को वास्तविक ठहराया गया था। कानून प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी के लिए एक उचित स्पष्टीकरण की मांग करता है, चाहे वह प्राथमिकी की जानकारी देनेवाले व्यक्ति की ओर से हो या पुलिस की ओर से। एक बलात्कार के मामले में, जहाँ अपराध होने के 10 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, देरी का यह कारण समझाया गया था कि इसमें पीड़िता के परिवार का सम्मान शामिल था, और इस प्रकार, परिवार के सदस्यों को यह तय करने में समय लगा कि क्या इस अपराध मामले में प्राथमिकी दर्ज करना उचित होगा या नहीं, न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को देरी के लिए एक उचित आधार के रूप में स्वीकार किया।
थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी
कुछ मामलों में, पुलिस घटना के बारे में पता लगाने के लिए पहले अपराध स्थल का दौरा करती है और बाद में उपस्थित गवाहों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करती है। यह पुलिस की ओर से गलत हो सकता है क्योंकि संज्ञेय अपराध के मामले में, पुलिस को पहले शिकायत दर्ज करनी चाहिए और फिर उसके पास मामले की जांच करने की शक्ति होती है। यह अत्यधिक देरी के बराबर है और प्राथमिकी को अत्यधिक देरी के आधार पर रद्द किए जाने की संभावना है। न्यायालय ने माना है कि जांच में अत्यधिक देरी के कारण प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।
तारा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में, न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के संबंध के कानून पर निम्नलिखित शब्दों में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया:
“प्राथमिकी देने में देरी अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकती है। भारतीय परिस्थितियों को जानते हुए, जैसा कि वे हैं, इन ग्रामीणों से घटना के तुरंत बाद पुलिस थाने जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मानव स्वभाव जैसा भी है, घटना के गवाह रहे रिश्तेदारों से पुलिस को सभी तत्परता के साथ यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कभी-कभी विपत्ति के कारण दुःखी होने के कारण उनके मन में यह तुरंत नहीं आता कि वे प्राथमिकी दर्ज करे। आखिरकार, इन परिस्थितियों में उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने जाने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। बेशक, तीव्र गुटों (एक्यूट फैक्शंस) से उत्पन्न होने वाले मामलों में, विपरीत गुट से संबंधित व्यक्तियों को झूठा फंसाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहराने के खतरे को टालने के लिए न्यायालयों को ऐसे इच्छुक गवाहों के साक्ष्य की अधिक सावधानी से जांच करने के लिए सावधान रहना चाहिए और सबूतों की बारीकी से जांच करने के बाद भूसी से अनाज को अलग करना चाहिए और ऐसा करने में प्राथमिकी की जानकारी की भी सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। हालाँकि, जब तक कि मनगढ़ंत संकेत न हों, न्यायालय प्राथमिकी में दिए गए अभियोजन पक्ष के संस्करण को अस्वीकार नहीं कर सकता है और बाद में केवल देरी के आधार पर सबूतों की पुष्टि करता है। ये सभी प्रशंसा के मामले हैं और बहुत कुछ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।”
मानव जीवन सबसे आवश्यक है और किसी घटना में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि पीड़ित जीवित रहे। पहले पुलिस थाने जाने के बजाय पीड़ित की जान बचाने के लिए अस्पताल जाना प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए एक संतोषजनक स्पष्टीकरण है।
यदि विलंब अस्पष्ट है और बहाने के आधार पर बस कुछ स्पष्ट कारण हैं, तो ऐसी देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक साबित हो सकती है। हालांकि, केवल देरी अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। कानून के इस नियम को कई मामलों में न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। रामदास और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “मात्र प्राथमिकी दर्ज करने में देरी अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है”। इसी तरह, हाल ही में, बंबई उच्च न्यायालय ने, एक बलात्कार के मामले में, यह माना कि एक बलात्कार पीड़ित द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकती है। इसके अलावा, केवल देरी ही अपने आप में संदेह का आधार नहीं हो सकती है कि प्राथमिकी विश्वसनीय नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे तत्परता यह मानने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि यह पूरी तरह से प्रामाणिक है। केसर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि प्राथमिकी दर्ज करने में 6 दिनों की देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। इस मामले में मृतक को चोटें आईं और छह दिन बाद मौत हो गई, मृतक इलाज के लिए अस्पताल में रहा, डॉक्टरों ने मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी।
न्यायाधीश को प्राथमिकी भेजने में देरी
कभी-कभी, प्राथमिकी कुछ प्रशासनिक कार्रवाइयों के कारण देर से न्यायाधीशतक पहुँचती है क्योंकि वे समय लेने वाली होती हैं और प्राथमिकी के लिए जानकारी देनेवाला और पुलिस दोनों के नियंत्रण से बाहर होती हैं। यदि प्रभारी अधिकारी की ओर से इस तरह की देरी की व्याख्या की जा सकती है, तो प्राथमिकी की विश्वसनीयता खुद ही बढ़ जाएगी। ऐसे मामले में जहां बाढ़ के कारण न्यायाधीश को रिपोर्ट भेजने में देरी हुई, न्यायालय ने कहा कि देरी को ठीक से बताया गया है और यह अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित नहीं हो सकती है। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी घातक होती है और इस तरह की देरी के कारण अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
- निम्नलिखित कुछ परिस्थितियाँ हैं जिन्हें प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण कहा जा सकता है। ये हैं:
- अभियुक्तों का डर (विलंब का मनोवैज्ञानिक कारण),
- परिवार के सम्मान के नुकसान का डर (विलंब का मनोवैज्ञानिक कारण),
- मुकदमा दर्ज करने में देरी,
- हत्या के कारण झटका लगना,
- मारपीट के कारण घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें आने की वजह से प्राथमिकी दायर करने में देरी (देरी का शारीरिक कारण),
- आरोपी को झूठ से फंसाने का मकसद,
- जब शिकायत में उल्लिखित तथ्यों को केवल देरी से नहीं बदला जा सकता है,
- उबड़-खाबड़ सड़क,
- खराब मौसम,
- परिवहन (ट्रांसपोर्ट) की अनुपलब्धता,
- जब सौहार्दपूर्ण समझौता (एमिकेबल सेटलमेंट) शुरू किया गया था।
राहीत हाजरा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में, अदालत के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज करने में अस्पष्ट विलंब एक कारण था जिसने अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं करने दिया।
प्राथमिकी दर्ज करने में उचित देरी की माफी
कई मामलों में देरी अभियोजन पक्ष के मामले को न्यायालय से बाहर ले आती है और न्यायालय को इस मामले को गंभीरता से देखना होता है ताकि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। न्याय के हित में प्राथमिकी दर्ज करने में सभी उचित देरी को माफ़ किया जाना चाहिए, और अभियुक्तों को तकनीकी चीजों और न्याय वितरण प्रणाली में देरी की रक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
कोई दूसरी प्राथमिकी
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और यह निर्धारित किया कि दूसरी प्राथमिकी नहीं हो सकती। मुखबिर के पहले बयान और कहानी को प्राथमिकी में दर्ज किया जाना चाहिए। और यदि कोई दूसरी शिकायत होती है, तो प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने का दायरा कम हो जाता है। न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि “पूछताछ के बाद हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है।” भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोकाब अली और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में दूसरी प्राथमिकी के विचार को बरकरार रखा था, जहां प्राथमिकी के पंजीकरण से पहले पूछताछ की गई थी। साथ ही दर्ज प्राथमिकी पंजीकरण के तीन दिन बाद न्यायाधीश तक पहुंची थी।
झूठी प्राथमिकी
देश, क्षेत्र या समाज पर ध्यान दिए बिना, झूठी शिकायत एक ऐसी घटना है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये झूठी प्राथमिकी किसी व्यक्ति को किसी मामले में फंसाने के लिए प्राथमिकी दायर करने वाले व्यक्ति या पुलिस द्वारा दर्ज कराया जा सकता है। झूठी प्राथमिकी के पंजीकरण से संबंधित मामले पहले वाले तरीके से अधिक पाए जाते हैं। भारतीय आपराधिक कानून के तहत, किसी के खिलाफ एक झूठी प्राथमिकी दर्ज करना भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और धारा 211 के तहत दंडनीय अपराध है।
धारा 182 किसी भी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को गलत सूचना देने पर छह महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है, जिसके आधार पर लोक सेवक कुछ ऐसी कार्रवाई करता है, जो उसने तथ्यों की सही स्थिति जानने के बाद नहीं की होती। दूसरी ओर, धारा 211 के तहत, ‘लोक सेवक’ शब्द का एक बार उपयोग होता है। इस प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो यह जानते हुए कि शिकायत और आरोप झूठे हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू करता है या करवाता है, वह एक अवधि के लिए कारावास का उत्तरदायी है जो दो साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा, यदि आरोप कथित अपराध का खुलासा करता है जो मौत की सजा है, या सात साल के लिए न्यूनतम कारावास है, तो अधिकतम 7 साल की कारावास की सजा दी जा सकती है।
अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि यदि वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दी गई शिकायत झूठी है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कार्यवाही शुरू करें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरभजन सिंह बाजवा बनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटियाला और अन्य के मामले में धारा 182 की विस्तृत व्याख्या दी गई है और यह बताया गया था कि:
“जब भी अधिकारियों को कोई सूचना दी जाती है और जब उक्त प्राधिकारी को पता चलता है कि शिकायत में किए गए आरोप झूठे थे, तो यह उक्त प्राधिकरण पर है कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कार्रवाई शुरू करे। भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत अपराध छह महीने की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है। जब 1996 और 1997 में उचित जांच के बाद अधिकारियों ने स्वयं पाया कि अश्विनी कुमार द्वारा उनकी शिकायत में किए गए दावे झूठे थे, तो यह उनके लिए तुरंत या निर्धारित अवधि के भीतर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए है। न्यायालय द्वारा रद्दीकरण रिपोर्ट की स्वीकृति सारहीन है। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के तहत सीमा को नहीं बचाता है। जो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय अपराध होने पर संज्ञान लेने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत अपराध केवल छह महीने की अवधि के कारावास के साथ दंडनीय है, इसलिए प्राधिकरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत जब उस प्राधिकारी ने पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोप झूठे थे उस तारीख से एक वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। चूंकि प्राधिकरण झूठे आरोप के बारे के पता चलने तक चार साल से अधिक समय बीत चुका है, तो ऐसे विलंबित अवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कोई शिकायत दर्ज करने का कोई सवाल ही नहीं होता है।”
मद्रास उच्च न्यायालय का विचार है कि प्राथमिकी के लिए जानकारी देनेवाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्राथमिकी का मुख्य उद्देश्य आपराधिक कानून को गति देना है और जांच अधिकारियों के दृष्टिकोण से इसे तुरंत रिकॉर्ड करना है ताकि अलंकरण के संबंध में पंजीकरण में देरी (यदि कोई हो), और अभियुक्तों को झूठ से फंसाने की संभावना के कारण के बारे में संदेह कम हो सके।
इस संबंध में, तुच्छ, क्षुद्र या मामूली प्रकृति के आधार पर शिकायतों की अनदेखी करने वाली पुलिस की कार्यशैली के दुष्परिणामों की संभावना को देखा जा सकता है। आजकल, लोग विवादों के अनौपचारिक समाधान की ओर झुकते हैं, और इसने किसी तरह पूरी शिकायत प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। इस प्रकार या तो मामले का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए या प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल) प्रक्रिया से एक बेहतर सौदा निकालने के उद्देश्य से, या जैसा कि अधिकारी ने आरोप लगाया कि किसी को झूठ से फंसाने के लिए, जनता कभी-कभी गलत तरीके से शिकायत में तथ्यों की गलत बयानी जैसे किसी विशेष घटना में किसी पर आरोप लगाना जैसे अनुचित व्यवहार में संलग्न हो सकती है। धारा 211 में एक वैधानिक निवारक (स्टेच्यूटरी डिटरेंट) है, लेकिन न्यायालयों ने कभी-कभी उस रास्ते को लेने से बचने का विकल्प चुना क्योंकि वे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं।
लेकिन, जैसा कि राजिंदर सिंह कटोच बनाम चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य के मामले में आयोजित किया गया था:
“यद्यपि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के संदर्भ में एक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी कानूनी रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य हैं, अगर उनके द्वारा लगाए गए आरोप एक अपराध को जन्म देते हैं जिसकी जांच बिना किसी अनुमति के की जा सकती है। संबंधित न्यायाधीश से; हालाँकि, यह किसी दिए गए मामले में प्रारंभिक जाँच करने के लिए सक्षम अधिकारी के अधिकार को छीन नहीं लेता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दर्ज की जाने वाली प्राथमिकी में कोई दम है या नहीं।”
न्यायपालिका ने कई मामलो में यह माना है कि,
- जब याचिकाकर्ता पुलिस के पास जाता है और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रार्थना करता है, तो एक संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध दर्ज करने के लिए पुलिस के वैधानिक कर्तव्य के अनुसार उन्हें प्राप्त होने वाले जानकारी को उसी रूप में दर्ज करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है और उसके बाद ही जांच शुरू होती है;
- पुलिस के पास कोई विवेक (डिस्क्रिशन) या अधिकार नहीं है कि
- मामला दर्ज करने से पहले वह दी गई जानकारी की विश्वसनीयता के बारे में पूछताछ करे, या
- इस आधार पर मामला दर्ज करने से इनकार करे कि यह नहीं है। जहाँ पुलिस ने झूठे आरोपों के आधार पर प्राप्त हुए एक लिखित अहवाल से प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया, जैसा कि उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय प्रारंभिक जाँच में निष्कर्ष निकाला गया था, की प्राथमिकी दर्ज करने और पूर्व पक्षीय प्रारंभिक जाँच (प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन) को गैर-प्रारंभिक जाँच मानते हुए नए सिरे से जाँच करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालयीन व्यवस्था ने यह अनुमान दिया है कि पुलिस को किसी मामले में या किसी शिकायत के आधार पर यह मानकर जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि मामला झूठा और मनगढ़ंत है।
न्यायालय ने संतोष बख्शी बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में फैसला सुनाते हुए धारा 182 के महत्वपूर्ण तत्वों पर चर्चा की है। वह यह कि:
- एक व्यक्ति द्वारा एक लोक सेवक को संबंधित सूचना के बारे जानकारी दी गई थी।
- जानकारी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई थी जो इस तरह के बयान को झूठा जानता या मानता है।
- ऐसी सूचना इस आशय से दी गई थी कि (a) ऐसे लोक सेवक को कुछ भी नहीं करना चाहिए, यदि तथ्यों की सही स्थिति जिसके संबंध में ऐसी जानकारी दी गई है, या
(b) किसी भी व्यक्ति को चोट या परेशान करने के लिए ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति का उपयोग करना।
उपचार (रेमेडी)
अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और वह यह भी जानता है कि यह झुटी और निराधार है, एहतियात के तौर पर उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए आवेदन (एप्लीकेशन) करने की स्वतंत्रता है। पीड़ित या आरोपी व्यक्ति न्यायालय में मानहानि के अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा, जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायत दर्ज की गई है, वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर सकता है। प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना इस आधार पर कि जा सकती है की
- प्राथमिकी में आरोपी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराए गए “कार्य” और “चूक” यह कोई अपराध नहीं है; या
- प्राथमिकी में कथित अपराध जैसी कोई घटना नहीं हुई है; या
- प्राथमिकी में आरोपी व्यक्ति की ओर से अपराध करने के लिए किसी भी “कार्य या चूक” को जिम्मेदार ठहराए बिना “झूठे आरोप” शामिल हैं।
भारत के विधि आयोग ने वर्ष 2012 में अपनी 243 वी रिपोर्ट में धारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 358 के तहत की झूठी/तुच्छ शिकायतों की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए जो कुछ लोगों के उत्पीड़न का कारण है और जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी होती है, इस प्रकार को रोकने के लिए धारा में संशोधन की सिफारिश की।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(a) के तहत, झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति पर उस लोक सेवक द्वारा, जिसके पास झूठी शिकायत की गई थी या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा, जिसे वह अधीनस्थ है इनके द्वारा उचित न्यायालय के सामने कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
प्राथमिकी को रद्द करना
भारतीय कानूनी प्रणाली ने उच्च न्यायालयों को एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई है, अगर वह न्यायालय इस बात पर संतुष्ट है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और कानून द्वारा प्रदान की गई शक्ति, अधिकारों और स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस तरह की कार्यवाही आवश्यक है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के वैध आधार पर प्राथमिकी को रद्द करने की शक्ति है। न्यायालयों की इन शक्तियों को ‘न्यायालय की निहित शक्तियाँ (इन्हेरेंट पावर)’ कहा जाता है।
देवेंद्र व अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामले में, यह माना गया था कि:
“अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उच्च न्यायालय आमतौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगे, अगर उन्हें लगे की प्राथमिकी में लगाए गए आरोप, भले ही वह अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) में दिए गए हों और उनकी संपूर्णता में सही हों, लेकिन वह कोई अपराध नहीं बनाते हो, और जब प्राथमिकी में लगाए गए आरोप या जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत, दी गई जानकारी को संतुष्ट नहीं करते हैं, ऐसे वक्त एक अपराध, न्यायपालिका एक आपराधिक न्यायालय में जो अपराध हुआ ही नहीं है उसके लिए न्यायालय के उत्पीड़न को प्रोत्साहित नहीं करेंगी। ”
इससे पहले, डॉ. शारदा प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य के मामले में यह कहा गया था कि:
“अब यह तय कानून है कि जहां शिकायत या आरोप पत्र (आरोप पत्र) में लगाए गए आरोप किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं; यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के लिए सक्षम है कि वह न्यायाधीश द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को रद्द कर दे।”
सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट किया जब कार्यवाही को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द किया जा सकता है। और यह निर्धारित किया कि निम्नलिखित मामलों में आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने वाले न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया जा सकता है:
- जहां शिकायत में लगाए गए आरोप या उसके समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया गया है, जिससे अभियुक्त के खिलाफ बिल्कुल कोई मामला नहीं बनता है या शिकायत जो आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया है उसके बारे में किसी अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है;
- जहां शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं ताकि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर न पहुंच सके कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है;
- जहां प्रक्रिया जारी करने में न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार या तो बिना किसी सबूत के या पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य जानकारी पर आधारित और मनमाना है; और
- जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोषों (फंडामेंटल लीगल डिफेक्ट्स) से ग्रस्त है, जैसे मंजूरी की इच्छा, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत की अनुपस्थिति और आदि।
हमारे द्वारा उल्लिखित मामले विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक हैं और उन आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जहां उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिसके अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है:
- जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके प्रारंभिक दिखने पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनता है।
- जहां प्राथमिकी में आरोप और अन्य जानकारी, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (1) या संहिता की धारा 155(2) के तहत एक न्यायाधीश के आदेश के तहत एक जांच को न्यायोचित (जस्टिफाईबल) ठहराया जा सकता है।
- जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए सबूत किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।
- जहां प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, न्यायाधीश के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत बताया गया है।
- जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है।
- जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही की निरंतरता और/या जहां संहिता में एक विशिष्ट प्रावधान है, के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है या संबंधित अधिनियम, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।
- जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लेती है और/या जहां अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के एक गुप्त उद्देश्य के साथ और एक निजी और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण उससे द्वेष रखने की दृष्टि से कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रूप से शुरू की जाती है।
न्यायालय ने माधवराव जीवाजी राव सिंधिया मामले में फैसला सुनाते हुए यह देखा है कि जहां मामले भी दीवानी प्रकृति के हैं, जैसे कि वैवाहिक, पारिवारिक विवाद आदि, न्यायालय “विशेष तथ्यों”, “विशेष विशेषताओं” पर विचार कर सकता है और पक्षों के बीच विवादों के वास्तविक समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
निहित शक्तियों की सीमा
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दी गई शक्तियां आपराधिक मामलों की न्यायिक समीक्षा जिस आधार पर टिकी है, उसे आधार बनाने के रूप में मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों की अंतर्निहित शक्तियों का एक लंबा और मजबूत प्रदर्शन किया है। इस संबंध में सामने आने वाली मूलभूत समस्या उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकारों को संवैधानिकता और वैधता की सीमाओं के भीतर रखना है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की अवमानना के अपराध के लिए एक वकील को दंडित कर सकता है। लेकिन एक वकील का लाइसेंस रद्द करना निहित शक्तियों का अत्यधिक उपयोग हो सकता है क्योंकि यह बार काउंसिल का कार्य है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति की कोई सीमा नहीं है। लेकिन, इस शक्ति का आह्वान करते समय अधिक शक्ति, अधिक उचित देखभाल और सावधानी बरती जानी चाहिए। उच्च न्यायालय की शक्तियों का गुरुत्वाकर्षण और दायरा निहित शक्तियों को लागू करने में संभावित सीमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है; आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 यह घोषणा करता है कि संहिता की कोई भी बात अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावित या सीमित नहीं करेगी। संहिता के तहत विशेष रूप से शामिल किए गए मामले अंतर्निहित शक्तियों से मुक्त हैं।