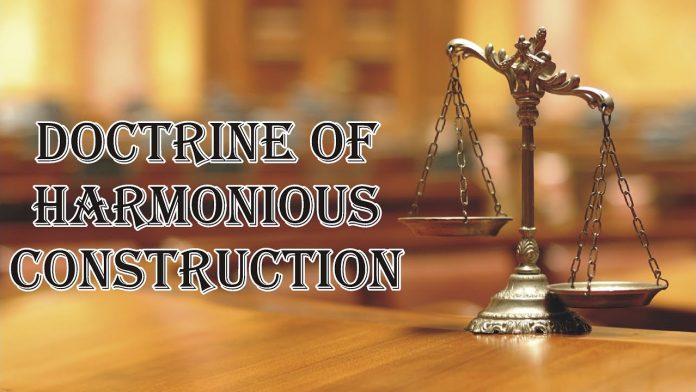यह लेख कोलकाता के एमिटी लॉ स्कूल के छात्र Aashutosh Sinh ने लिखा है। यह लेख कई मामलों के उपयोग के साथ सामंजस्यपूर्ण निर्माण (हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन) के सिद्धांत की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
एक कानूनी सिद्धांत एक सिद्धांत या एक स्थिति है जिसे आमतौर पर अदालतों द्वारा लागू और बरकरार रखा जाता है। न्यायपालिका द्वारा विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर भारतीय संवैधानिक कानून में समय के साथ विभिन्न न्यायिक सिद्धांत विकसित हुए हैं। ये कानूनी अवधारणाएं एक बार में नहीं बनाई गई है, लेकिन वे असहमति, अशांति, बहस और विधायी समाधानों का परिणाम हैं, और इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये स्थितियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब क़ानून में अस्पष्टता के कारण क़ानून और उनके प्रावधानों की एक से अधिक व्याख्याएँ होती हैं। क़ानून के अधिनियमित होने के बाद, विधायिका कार्यकारिणी (फंक्टस ऑफिशियो) (अब अधिकार क्षेत्र नहीं है) बन जाती है। कानून के दुभाषिए (इंटरप्रेटर्स) तब सवाल करने में असमर्थ होते हैं या विधायिका के पास वापस जाकर कानून की सटीक व्याख्या का अनुरोध करने में असमर्थ होते हैं, जब वे इसे बना रहे थे। कभी-कभी कानून निर्माताओं ने किसी भी क़ानून का मसौदा तैयार करते समय परिस्थितियों की इतनी विस्तृत श्रृंखला पर इतना विचार नहीं किया होगा। किसी भी क़ानून की व्याख्या के लिए थंब रूल तब सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम है।
सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का पालन तब किया जाता है जब दो या दो से अधिक विधियों या किसी विशेष क़ानून के अनुभागों के बीच असंगति (इनकंसिस्टेंसी) उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत के पीछे मूल सिद्धांत है, एक क़ानून का एक कानूनी उद्देश्य होता है जिसे पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए और उसके बाद, उस क़ानून के सभी प्रावधानों के अनुरूप व्याख्या का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहां सभी खंडों में सामंजस्य स्थापित करना संभव नहीं है, तब ऐसे समय उस प्रावधान पर अदालत के फैसले को प्राथमिकता दी जाती है।
सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के पीछे का इतिहास
सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत विभिन्न मामलों में विभिन्न क़ानूनों की कई अलग-अलग अदालती व्याख्याओं के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया है। समय-समय पर, न्यायपालिका ने उन मामलों का फैसला किया है, जिनमें दो अलग-अलग प्रावधानों के बीच विरोध शामिल था। यह सिद्धांत पहले सेंट्रल प्रोविएन्स और बरार अधिनियम (1939) के मामले में सुलह के नियम के रूप में सामने आया था, जहां शामिल अदालत ने भारतीय संविधान में सूची I की प्रविष्टि (एंट्री) और सूची II की प्रविष्टि के बीच विसंगति (डिस्क्रिपेंसी) को हल किया और उनकी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की थी।
ऊपर बताए हुए मामले में, सवाल यह था कि क्या एक प्रांतीय विधायिका द्वारा तेल की बिक्री पर कर इसे बनाने वाले व्यक्ति द्वारा इस आधार पर लगाया गया था कि यह वास्तव में एक उत्पाद शुल्क था। फिर, एक प्रांतीय विधायिका द्वारा बिक्री कर लगाया जा सकता था, और उत्पाद शुल्क केवल संघ विधायिका द्वारा लगाया जा सकता था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह अजीब होगा यदि संघ के पास खुदरा (रिटेल) बिक्री पर कर लगाने की अनन्य शक्ति होती है, जब प्रांत के पास व्यापार और वाणिज्य, इसके उत्पादन और आपूर्ति (सप्लाई) और माल के वितरण के संबंध में कानून बनाने की कार्यकारी शक्ति होती है लेकिन वह इसकी सीमाओं के भीतर होती है। इसलिए, यह एक बिक्री कर था और अधिनियम अल्ट्रा वायर्स नहीं था। न्यायालय ने कहा कि दो प्रविष्टियों में कोई अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) या संघर्ष नहीं था, जिसकी वजह से एक गैर-बाधा खंड लागू किया जा सकता है।
श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ (1951) के ऐतिहासिक निर्णय में, सिद्धांत की अवधारणा को भारत के संविधान के पहले संशोधन, 1951 में सभी तरह से ट्रैक किया जा सकता है। जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों (भाग III) और निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) के बीच असहमति के मामले का विषय थी। संवैधानिक कानून मुख्य रूप से तीन महान अंगों के निर्माण और उनके बीच सरकारी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, जो कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है।
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम का उपयोग किया और माना कि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ दिए गए हैं और उन्हें केवल कुछ परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है और यहां तक कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए संसद द्वारा संशोधित भी किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को प्राथमिकता देते हुए कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उनका एक साथ काम करना उनके लिए फायदेमंद होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मौलिक अधिकार विधायिका और कार्यकारी शक्ति दोनों पर सीमा लागू करते हैं। वे पवित्र नहीं हैं और संसद उन्हें निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप लाने के लिए उनमें संशोधन कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने रे केरल एजुकेशन बिल केस (1957) मामले में सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच कोई अंतर्निहित संघर्ष नहीं था और वे एक साथ एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक एकीकृत योजना और एक व्यापक प्रशासनिक और सामाजिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। न्यायालय ने उन्हें एक-दूसरे का पूरक (सप्लीमेंट) बताया है। इसलिए, उन्हें सामंजस्यपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि अदालतें मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष से बच सकें। वे मूल रूप से एक दूसरे के समानांतर चलते हैं और कोई भी एक दूसरे के अधीनस्थ (सबॉर्डिनेट) नहीं है।
सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का दायरा और उद्देश्य
न्यायपालिका और न्यायालयों का उद्देश्य कानून को समग्र रूप से देखना होना चाहिए। कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि यह इस्तेमाल किए जा रहे क़ानून के विभिन्न वर्गों या भागों के बीच भ्रम या असंगति को रोके। जब भी दो या दो से अधिक विधियों या किसी क़ानून के विभिन्न खंडों या वर्गों के बीच कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यह सीधे सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक क़ानून का एक कानूनी उद्देश्य होता है और इसे समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए। व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि वह अटल हो और क़ानून के सभी प्रावधानों का उपयोग भी किया जाना चाहिए। इस घटना में कि दो या दो से अधिक विधियों या किसी क़ानून के अलग-अलग खंड या अनुभागों का सामंजस्य संभव नहीं है, इस प्रावधान पर अदालत के फैसले को प्राथमिकता दी जाएगी।
सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत से संबंधित लैटिन मैक्सिम्स
जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगंट
इस लैटिन मैक्सिम का अर्थ है कि जब भी प्रावधान खतरे में होते हैं, तो अदालतें सामान्य आवेदन के प्रावधानों के लिए विशिष्ट प्रावधानों को प्राथमिकता देती हैं। दूसरे शब्दों में, दो विधियों के बीच संघर्ष के मामले में पालन किया जाने वाला सामान्य नियम यह है कि नया आया हुआ प्रावधान पिछले वाले को वापस ले लेता है। कोई भी उस पिछले या विशेष विधान को अप्रत्यक्ष रूप से निरस्त (रीपील), परिवर्तित (अल्टर) या ऐसा करने के विशेष इरादे के किसी भी सुझाव के बिना, केवल ऐसे सामान्य शब्दों के उपयोग से इसे डेरोगंट नहीं मान सकता है। इसका मतलब यह है कि एक पूर्व विशेष कानून बाद के सामान्य कानून में बदल जाएगा यदि निम्नलिखित में से दो शर्तें पूरी होती हैं, तो बाद का कानून, भले ही सामान्य हो, लेकिन प्रबल होगा यदि:
- दोनों प्रावधान एक दूसरे के विरोधी हैं।
- पिछले अधिनियम के बाद के विधान में कुछ स्पष्ट संदर्भ है।
जनरलीबस स्पेशलिया डेरोगंट
जनरलीबस स्पेशलिया डेरोगंट भारत में सामंजस्यपूर्ण निर्माण नियम के संबंध में इस्तेमाल किए जाने वाली एक और कानूनी कहावत है। इसका मूल रूप से मतलब है कि विशेष चीजें सामान्य चीजों से अलग हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विशेष विषय पर विशेष प्रावधान किया जाता है, तो उससे संबंधित मामलो को सामान्य प्रावधानों से बाहर रखा जाता है। इस नियम को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने विनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (2003) के अपने फैसले में कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 351 भारत में हिंदी के विकास के संबंध में एक सामान्य प्रावधान है। अनुच्छेद 348 दूसरी ओर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 351 की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) पूरी तरह से रोकी गई है।
सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत
आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स हिंदुस्तान थोक वाहक (2000) एक ऐतिहासिक मामला है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने पांच मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए जो सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को नियंत्रित करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:
- न्यायालयों को प्रतीत होता है कि विवादित प्रावधानों के टकराव से बचने की कोशिश करनी चाहिए और विवादित प्रावधानों को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि उनमें सामंजस्य बनाया जा सके।
- एक खंड के प्रावधान का उपयोग दूसरे खंड में शामिल प्रावधान को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि अदालत अपने सभी प्रयासों के बावजूद अपने मतभेदों को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेती है।
- ऐसी स्थिति में जब अदालत को असंगत प्रावधानों में मतभेदों को पूरी तरह से सुलझाना असंभव लगता है, ऐसे समय में अदालतों को उनकी व्याख्या इस तरह करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो दोनों प्रावधानों को प्रभाव दिया जा सके।
- न्यायालयों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्याख्या जो एक प्रावधान को अनावश्यक और बेकार बनाती है, वह सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सार के खिलाफ है।
- दो परस्पर विरोधी प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ है किसी भी वैधानिक प्रावधान को नष्ट न करना या इसे अप्रभावी बनाना।
सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का अनुप्रयोग
न्यायालयों ने कई मामले कानूनों की समीक्षा के बाद पूर्वोक्त सिद्धांत की उचित प्रयोज्यता के लिए कुछ प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है। वे इस प्रकार हैं:
- दोनों परस्पर विरोधी प्रावधानों को समान महत्व देना, और इस प्रकार उनकी असंगति को कम करना।
- जो प्रावधान मौलिक रूप से असंगत या एक-दूसरे के प्रतिकूल (रिपग्नेंट) हैं, उन्हें उनकी संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए, और पूर्ण अधिनियम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- दो विरोधाभासी (कॉन्ट्रेडिक्टिंग) प्रावधानों की व्यापक पहुंच वाले प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए।
- व्यापक और संकीर्ण (नैरो) प्रावधानों की तुलना करते हुए, अदालतों को यह देखने के लिए व्यापक कानून का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या कोई अन्य चिंताएं हैं। यदि परिणाम उचित हो तो और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है और दोनों खंडों को अलग-अलग भार देकर सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका उस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी, जिससे वे प्रावधानों को अधिनियमित करते समय संबोधित करने का प्रयास कर रहे थे, और इसलिए अपनाए गए सभी प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए।
- जब अधिनियम के एक प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो दूसरे अधिनियम द्वारा दिए गए शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- यह महत्वपूर्ण है कि अदालत उस डिग्री को स्थापित/ साबित करे, जिसकी वजह से विधायिका एक प्रावधान को दूसरे पर अधिभावी (ओवरराइडिंग) अधिकार देना चाहती थी।
सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत के आवेदन की व्याख्या करने वाले मामले
कुछ प्रसिद्ध भारतीय मामले निम्नलिखित हैं, जहां अदालतों ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करने की सहायता से कुछ विधियों की व्याख्या करने का प्रयास किया है।
श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति बनाम सिद्ध मठ और अन्य (2015)
इस मामले में, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 और उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, (ओईए) 1951 के प्रावधान जांच में आए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 की धारा 2 (oo) और श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 30 के बीच एक स्पष्ट संघर्ष उत्पन्न हुआ है। अदालत ने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि दोनों दिए गए वैधानिक उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधान एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम का उपयोग करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब दो विधियों के प्रावधान असंगत हों, तो यह तय करना होगा कि किस प्रावधान को प्रभावी किया जाना चाहिए।
इस मामले में, उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम की धारा 2(oo) अपनी संपूर्णता में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर रही थी। यह प्रावधान का केवल पहला भाग था जो जगन्नाथ मंदिर अधिनियम का खंडन कर रहा था। यदि प्रावधान के उस भाग को लागू करना जारी रखा जाता है तो जगन्नाथ मंदिर अधिनियम की धारा 5 और धारा 30, जिसके द्वारा पुरी में जगन्नाथ मंदिर की सम्पदा को मंदिर समिति को सौंपा जाता है, अपना अर्थ खो देगी। न्यायालय ने आगे बताया कि उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम की धारा 2(oo) के प्रावधान को समाप्त करने से दोनों प्रावधान लागू होंगे। जब भी एक ही मामले में विशिष्ट और सामान्य कानूनों के लागू होने के बारे में कोई प्रश्न आता है, तो मामले की प्रकृति और मुद्दों की संबंधित अदालत द्वारा जांच की जानी चाहिए। यदि, दो कानून पूर्ण संघर्ष में हैं, तो विधायिका द्वारा लगाई गई सीमाओं और अपवादों पर एक जांच होनी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के विशेष प्रावधान प्रबल होंगे, और इस प्रकार, जनरलिया स्पेशलिबस डेरोगेंट के सिद्धांत को लागू किया जाएगा।
वेंकटरमन देवरु बनाम मैसूर राज्य (1957)
इस मामले में, श्री वेंकटरमण के एक प्राचीन, प्रसिद्ध मंदिर के ट्रस्टियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 92 के तहत एक मुकदमा दायर किया, जिसमें प्राधिकरण अधिनियम (1947 का मद्रास V) के पारित होने के बाद मद्रास मंदिर प्रवेश के बाद हरिजनों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। ट्रस्टियों ने सरकार को एक प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) दिया कि मंदिर निजी था और विशेष रूप से गौड़ा सारस्वथ ब्राह्मणों के लिए स्थापित किया गया था, और इसलिए, मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम के संचालन के बाहर था। हालांकि, सरकार ने उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया और माना कि उक्त अधिनियम मंदिर पर लागू होता है।
ट्रस्टियों ने तर्क दिया कि मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2 (2) के तहत मंदिर को परिभाषित नहीं किया गया था और अधिनियम की धारा 3 शून्य थी क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 (b) के लिए अपमानजनक था। इस प्रकार, निचली अदालत में अपील की गई, जिसने अपीलकर्ताओं के खिलाफ फैसला सुनाया। लेकिन मद्रास के उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक सीमित डिक्री पारित करते हुए कहा कि हालांकि आम तौर पर जनता, मंदिर में पूजा करने की हकदार थी, अपीलकर्ताओं को कुछ समारोहों के दौरान आम जनता को बाहर करने का अधिकार था, जिसमें केवल अकेले गौड़ा सारस्वत ब्राह्मणों के सदस्य भाग लेने के हकदार थे। इस विवाद से निपटना कि मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 (b) का उल्लंघन है, संविधान का अनुच्छेद 25 (2) (b) लागू होगा, और इसलिए, हिंदुओं के सभी वर्गों को पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार था।
न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25(1) व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 26(b) धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों से संबंधित है। हालाँकि, अनुच्छेद 25(2) एक बहुत व्यापक आधार को शामिल करता है और दोनों अनुच्छेद को नियंत्रित करता है। इसलिए अनुच्छेद 26(b) को संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने मद्रास मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम (1947 के V) की धारा 2 (2) और धारा 3 की व्याख्या में अड़चनों को स्पष्ट करते हुए धर्म के मामले और उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं के सामंजस्य से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2)(b) और अनुच्छेद 26(b) की व्याख्या के समय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील और अपील के लिए विशेष अनुमति के आवेदन दोनों को खारिज कर दिया।
राजस्थान राज्य बनाम गोपी किशन सेन (1992)
इस मामले में प्रतिवादी को, 1972 में राजस्थान में एक अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। राजस्थान राज्य, जो अपीलकर्ता है, उन्होंने इस मामले में रुपये 160-360/- प्रति माह के वेतनमान पर उसके वेतन के दावे को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद प्रतिवादी ने राजस्थान के उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन किया, जिसे आक्षेपित निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी। हालांकि वेतनमान रु. 160-360/- प्रति माह केवल प्रशिक्षित शिक्षकों को ही दिया जाता था। प्रतिवादी एक प्रशिक्षित शिक्षक नहीं था और इसलिए, उसे रुपये 130/- प्रति माह के निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया था, जब तक कि वह प्रशिक्षित नहीं हो जाता, जो राजस्थान सिविल सेवा (नए वेतनमान) नियम, 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, जिसे राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के साथ पढ़ा जाता है।
हालांकि बाद में वेतनमान में संशोधन किया गया है। प्रति माह रुपये 130/- की राशि अप्रशिक्षित शिक्षक के वेतन के रूप में निर्धारित की गई थी और इस प्रावधान को अवैध भेदभाव मानते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। तदनुसार, अपीलकर्ता को प्रतिवादी को 1972 से 1982 की अवधि के लिए उच्च दर पर उसका वेतन देने के लिए कहा गया था और इसे अपीलकर्ता की ओर से त्रुटिपूर्ण के रूप में चुनौती दी गई थी।
जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो न्यायालय ने देखा कि प्रतीत होता है कि विरोधाभासी वैधानिक प्रावधानों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है, जहां तक संभव हो, सभी प्रावधानों को बनाए रखने और प्रभावी बनाने और व्याख्या से बचने के लिए जो किसी को भी शक्तिहीन बना सकता है।
वेतनमान में वृद्धि से संबंधित राजस्थान सेवा नियम, 1951 का नियम 29 सामान्य शब्दों में है, जबकि राजस्थान सिविल सेवा (नया वेतनमान) नियम, 1969 की अनुसूची में अप्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख का एक विशेष प्रावधान है। इस प्रकार यह मामला अधिकतम ‘जनरलिबस स्पेशलिया डेरोगंट’ को आकर्षित करता है क्योंकि जब किसी निश्चित विषय पर विशेष प्रावधान किया जाता है, तो उस विषय को सामान्य प्रावधान से बाहर रखा जाता है।
उन्नी कृष्णन, जेपी, आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1993)
उन्नी कृष्णन का मामला भारत में शिक्षा के अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए ‘जीवन के अधिकार’ के प्रश्न को चुनौती दी थी। अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो मुद्दे आए, वे थे, क्या किसी नागरिक के पास चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि जैसी व्यावसायिक डिग्री के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार है और क्या हमारा संविधान अपने सभी नागरिकों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।
एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें चुनौती दी गई थी कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन का अधिकार’ भारत के सभी नागरिकों को शिक्षा के अधिकार में शामिल करता है और गारंटी देता है, और यहां शिक्षा के अधिकार में व्यावसायिक शिक्षा या डिग्री भी शामिल है।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इसमें बुनियादी शिक्षा के अधिकार का अनुमान लगाया गया था: जैसे की शिक्षा पर निर्देशक सिद्धांत (डायरेक्टिव प्रिंसिपल) के अनुच्छेद 41 के साथ पढ़े जाने पर अनुच्छेद 21 के तहत दीया गया जीवन का अधिकार। न्यायालय ने अनुच्छेद 45 का भी उल्लेख किया और अनुमान लगाया कि अनुच्छेद 21 से निकलने वाली पेशेवर डिग्री के लिए शिक्षा का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ़ स्टेट पॉलिसी) (डीपीएसपी) पर मौलिक अधिकारों के प्रसार के मुद्दे पर, न्यायालय ने टिप्पणी की कि भाग तीन और भाग चार के प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं और मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए क्योंकि वे भारतीय संविधान के सामाजिक विवेक (सोशल कॉन्सिएंस) का निर्माण करते हैं।
सिरसिल्क बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (1963)
इस मामले में सिरसिल्क कंपनी का आंध्र प्रदेश सरकार और उनके कर्मचारियों से विवाद हो गया था। विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण (इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल) में भी ले जाया गया। इस पर निर्णय लेने के बाद, प्राधिकरण ने सितंबर 1957 में अपना निर्णय दिया जिसके बाद इसे आंध्र प्रदेश सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाना था। लेकिन निगम (कॉर्पोरेशन) और कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से निर्णय को प्रकाशित नहीं करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी असहमति को मित्रतापूर्ण ढंग से सुलझा लिया था। सरकार ने पक्षों की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसके बाद पक्षों ने एक प्रकाशन में निर्णय के मुद्दे को प्रकाशित करने से रोकने के लिए सरकार को एक आदेश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ एक रिट आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने रिट आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17 के तहत अनिवार्य और औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा सरकार को सौंपे गए निर्णय के पारित होने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। तब सिरसिल्क कंपनी के पक्षों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी।
निगम और कर्मचारियों ने प्रस्तुत किया कि चूंकि दोनों पक्षों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 18 (1) के तहत उनके लिए बाध्यकारी है, धारा 17 (1) के तहत सरकार का निर्णय, समूह के लिए चुनौतीपूर्ण है और इसलिए इन्हें जारी नहीं किया जाना चाहिए। पक्षों द्वारा सहमती से दिए गए संकल्प (आइडिया) का पालन किया जाना चाहिए और औद्योगिक शांति बनाई रखी जानी चाहिए। दूसरी ओर, सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17 (1) की अनिवार्य प्रकृति के बारे में बताते हुए कहा कि निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसे जारी किया जाना था। न्यायाधिकरण के संदर्भ का उद्देश्य विवादों का निपटारा करना है और जब पक्षों के बीच एक समाधान हो जाता है तो न्यायाधिकरण द्वारा जारी प्रकाशन के लिए निर्णय का प्रश्न अतार्किक (इल्लॉजिकल) प्रतीत होता है और इसका कोई सार नहीं है क्योंकि न्याधिकरण के निर्णय द्वारा प्रदान किए गए हल का कोई संघर्ष अब बचा नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के बीच मतभेद है और एक उपाय खोजना महत्वपूर्ण है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्राथमिक स्पेक्ट्रम को संरक्षित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस तरह के मामले के दो विरोधाभासी खंडों को हल करने का एकमात्र तरीका सरकार को निर्णय के प्रकाशन को वापस लेने की अनुमति देना और पक्षों को अपने संकल्प को जारी रखने की अनुमति देना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जबकि अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 अनिवार्य थी, इस तथ्य के बावजूद पक्षों ने पहले ही समझौते से अपने विवाद को मित्रतापूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, लेकिन वर्तमान मामले में, कोई भी विवाद प्रकाशन द्वारा हल नहीं किया गया है। और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अधिनियम 17(1) के अनुपालन में निर्णय को प्रकाशित न करने का निर्देश दिया और अपील को मंजूरी दे दी गई।
सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे एक प्रावधान के नियम कानून के दूसरे प्रावधान को अर्थहीन या अप्रचलित किए बिना लागू किए जा सकता है।
के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1961)
यह भारतीय कानूनी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक है और भारत में इस मामले के बाद जूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया गया था। एक नौसेना कमांडर के. एम. नानावती पर अपनी पत्नी के गुप्त प्रेमी प्रेम आहूजा की हत्या का आरोप लगाया गया था, और परिणामस्वरूप, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था।
उन पर आईपीसी की धारा 302 और धारा 304 के तहत आरोप लगाया गया था और एक सत्र न्यायाधीश, बॉम्बे द्वारा मुकदमा चलाया गया था और विशेष जूरी ने उन्हें आईपीसी के तहत शामिल दोनों धाराओं के तहत दोषी नहीं ठहराया था। हालांकि, सत्र न्यायाधीश जूरी के फैसले से असंतुष्ट थे क्योंकि उन्हें लगा कि मामले के सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह तार्किक निर्णय नहीं था। इसलिए, वह आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 307 के तहत मामले को अपने विचारों का कारण देते हुए बॉम्बे के उच्च न्यायालय में ले गए। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के तर्क को मंजूरी दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपराध को हत्या से गैर इरादतन हत्या में शामिल नहीं किया जा सकता, जो कि हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। उच्च न्यायालय ने नानावती को हत्या के अपराध का दोषी ठहराया और इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में आगे चुनौती दी गई। इस बीच, बॉम्बे के गवर्नर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत निहित शक्ति का उपयोग करके नानावती के निलंबन (सस्पेंशन) का आदेश पारित किया।
राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाया गया था क्योंकि जब निलंबन का आदेश दिया गया था, तो मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन (सब जुडिस) था। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच उत्पन्न हुए संघर्ष को सुलझाने के लिए सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 और राज्यपाल द्वारा निलंबन तब लागू नहीं होता जब मामला विचाराधीन हो।
कलकत्ता गैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1962)
ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, 1960 पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इस मामले में, अपीलकर्ता ने इस अधिनियम की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि राज्य विधान सभा को राज्य के प्रवेश 24 और प्रविष्टि 25 (भारत का संविधान, सूची II) के तहत ऐसा अधिनियम पारित करने की कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि सरकार कंपनी के प्रबंधन को संभालना चाहती थी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संसद पहले ही उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 को संघ सूची/ सूची I की प्रविष्टि 52 के तहत अधिनियमित कर चुकी है, जो उद्योगों से संबंधित है।
राज्य सूची में संपूर्ण उद्योग प्रविष्टि 24 के अंतर्गत आते हैं, और प्रविष्टि 25 केवल गैस उद्योग तक ही सीमित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम का इस्तेमाल किया और कहा कि यह स्पष्ट था कि गैस उद्योग पूरी तरह से राज्य सूची की प्रविष्टि 25 द्वारा कवर किया गया था, जिस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। इसलिए, राज्य के पास इस संबंध में कानून बनाने की शक्ति थी। इसलिए, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम की मदद से, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त किया कि गैस उद्योग प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है जो राज्य सूची का एक हिस्सा है, और यह राज्य को इस पर पूर्ण नियंत्रण देता है।
निष्कर्ष
भारत में न्यायपालिका और अदालतें एक उपकरण के रूप में सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का उपयोग करके भारतीय संविधान के हर प्रावधान के उद्देश्य की रक्षा और रखरखाव के लिए सभी प्रयास कर रही हैं। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न विधियों को बनाने के लिए संविधान निर्माताओं के इरादे या उद्देश्य को समझाने की कोशिश की है। इस लेख में विभिन्न मामलों के विश्लेषण के माध्यम से, यह कहा जा सकता है की सामंजस्यपूर्ण निर्माण का नियम विभिन्न परस्पर विरोधी प्रावधानों के बीच एकरूपता (यूनिफॉर्मिटी) लाता है ताकि उनमें से कोई भी शक्तिहीन या मृत-अक्षर न हो क्योंकि उन्हें बनाने में विधायिका द्वारा काफी विचार किया जाता है।
संदर्भ