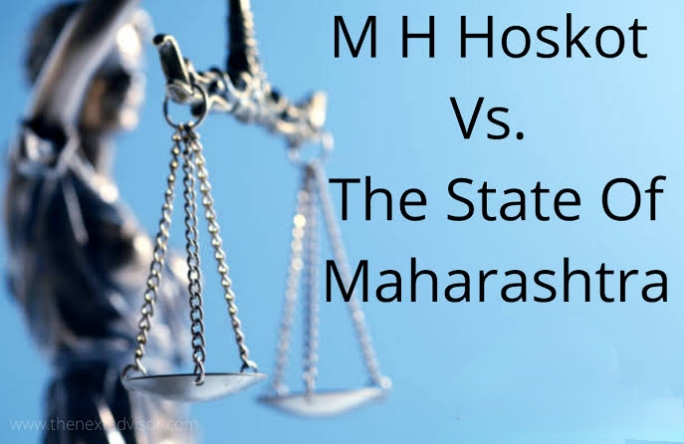यह लेख Debapriya Biswas द्वारा लिखा गया है। यह लेख एमएच होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) के ऐतिहासिक मामले के विश्लेषण से संबंधित है। इसके अलावा, लेख मामले में उठाए गए मुद्दों और इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर चर्चा करता है। अंत में, लेख निर्णय के महत्व के साथ-साथ वर्तमान समय में भी इसके भविष्य के निहितार्थों का पता लगाता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारत के संविधान के भाग III में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। हर व्यक्ति इन अधिकारों का हकदार है, चाहे उसकी उम्र, लिंग, जाति, स्थिति, वर्ग आदि कुछ भी हो। हालांकि, गारंटी के बावजूद, जेलों में बंद व्यक्तियों को अक्सर मौलिक अधिकारों के सबसे ज़्यादा उल्लंघन का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कई की रिपोर्ट भी नहीं की जाती है।
किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाना और उसके अपराधों के लिए दोषी पाया जाना, किसी व्यक्ति की हैसियत को व्यक्ति से गैर-व्यक्ति में गिरा देने के बराबर नहीं है। हर व्यक्ति बुनियादी मानवाधिकारों का हकदार है और इसलिए जेल में बंद व्यक्ति भी। एमएच होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) के ऐतिहासिक फैसले में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें कैदी के बुनियादी अधिकारों के साथ-साथ उन कैदियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और सहायता की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई है जो कानूनी सेवाएं हासिल करने में असमर्थ हैं।
मामले का विवरण
फैसले की तारीख
17 अगस्त, 1978
मामले के पक्ष
याचिकाकर्ता: माधव हयावदनराव होसकोट
प्रतिवादी: महाराष्ट्र राज्य
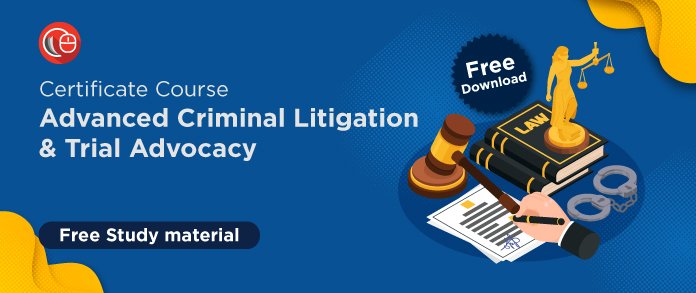
उद्धरण
1978 एआईआर 1548, 1979 एससीआर (1) 192, 1978 एससीसी (3) 544, एआईआर 1978 सर्वोच्च न्यायालय 1548, 1978 एससीसी (सीआरआई) 468।
अदालत
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
न्यायाधीश
- माननीय न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्ण अय्यर
- माननीय न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई
- माननीय न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी
मामले की पृष्ठभूमि
भारत में शिक्षा का मतलब सिर्फ़ ज्ञान की खोज से कहीं ज़्यादा है – इसे आगे के अवसरों के द्वार के रूप में देखा जा सकता है या यहाँ तक कि खुद एक अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है, जो उच्च वेतन वाली नौकरी पाने में मदद करता है। किसी प्रतिष्ठित कॉलेज या विश्वविद्यालय से शिक्षा का स्तर जितना ऊँचा होगा, उच्च वेतन वाली नौकरियों के लिए चुने जाने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी।
डिग्रियों के लिए इतनी भूख के साथ, भारतीय समुदाय ऐसी डिग्रियों के जालसाजी के लिए एक बहुत ही अनुकूल शिकारगाह प्रदान करता है, जैसा कि याचिकाकर्ता के वर्तमान मामले में देखा गया है। यदि इस तरह के निर्माण में विशेषज्ञता किसी अन्य ललित कला की तरह निपुण है और अधिकारियों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जाता है, तो इस अनैतिक व्यवसाय में एक ईमानदार डॉक्टरेट की तुलना में काफी अधिक गुंजाइश है।
वर्तमान नौकरी परिदृश्य में भी, एक ही नौकरी की पोस्टिंग के लिए प्रतिस्पर्धा (कंपटीशन) बहुत अधिक है, भले ही वेतन बाजार दर से काफी कम हो। बेरोजगारी की दर अधिक है और लोग हताश हैं। ऐसी परिस्थितियों में, अधिकांश लोग या तो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों को उच्चतम डिग्री तक बढ़ाने का प्रयास करते हैं या संदर्भों के माध्यम से काम ढूंढते हैं। चूंकि अधिकांश लोग पूर्व श्रेणी में आते हैं, इसलिए डिग्री और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का निर्माण भी अपना रास्ता खोज लेता है।
इसके अलावा, शिक्षा महंगी है, खासकर स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन जैसी उच्च शिक्षा। ये दोनों महंगी हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। जबकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो वाले लोगों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है, कई लोगों को प्रत्येक सीट के लिए उच्च प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसे संस्थानों में प्रवेश मिलना भी मुश्किल लगता है।
इस प्रकार, लोगों को या तो दाखिला लेने और रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं या फिर आगे पढ़ने का सपना छोड़ देना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी डिग्री को नकली बनाने का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि यह एक सस्ता लेकिन अनैतिक विकल्प है।
मूलतः, जबकि शिक्षा अभी भी एक आवश्यकता है, शिक्षा प्रणाली एक सीमा रेखा घोटाला बन गई है – यह दृष्टिकोण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्तमान निर्णय में व्यक्त किया है।
सामाजिक पृष्ठभूमि
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता पीएचडी और एमएससी धारक है, जबकि वह उसी कॉलेज से उसी स्तर की जली डिग्री बनाने का प्रयास कर रहा है, जहां से उसने ये डिग्री हासिल की थी – यह एक विडंबना है जो मनोरंजक से अधिक दुखद है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो उस समय बुनियादी स्कूली शिक्षा से आगे की शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं था।
इस प्रकार, याचिकाकर्ता की उच्च शैक्षणिक पृष्ठभूमि और उसकी आर्थिक स्थिति एक ऐसी छवि प्रस्तुत करती है जो कई लोगों के लिए पहले से ही परिचित है। अक्सर यह अपेक्षा की जाती है कि किसी के पास जितनी अधिक डिग्री होगी, उसे उतनी ही अधिक वेतन वाली नौकरी मिलेगी, लेकिन वर्तमान मामले से यह स्पष्ट होता है कि यह सोच पूरी तरह सच नहीं है।
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शिक्षा प्रणाली अपनी महंगी कीमत और उपलब्धता से अधिक मांग के कारण सीमा रेखा पर घोटाला बन गई है। इसने कई घोटालेबाजों को पैसे कमाने के लिए डिग्री बनाने और बेचने के लिए प्रेरित किया है, जो अक्सर एक ईमानदार डॉक्टरेट से भी अधिक पैसा कमाते हैं। वर्तमान मामले के याचिकाकर्ता ने भी यही सोचा था क्योंकि उसने कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री के प्रमाण पत्र के निर्माण का प्रयास किया था। हालाँकि, ऐसा करने से पहले ही उसे पकड़ लिया गया और उस पर प्राधिकरण पत्रों की जालसाजी और उसके धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया।
अन्य अपराधों की तरह गंभीर न होते हुए भी, उपरोक्त अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालाँकि शुरू में याचिकाकर्ता को उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि और प्रेरणा को देखते हुए बहुत हल्की सज़ा दी गई थी, लेकिन जल्द ही इसे संशोधित कर तीन साल की कैद तक बढ़ा दिया गया।
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिति चर्चा के मुख्य बिंदुओं में से एक बन गई, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की प्रति की सेवा में देरी के कारण उसे अपील करने के अपने अधिकार से वंचित किया गया था, साथ ही उसके पास कानूनी पेशेवर को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं था। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए, याचिकाकर्ता ने अपनी सजा समाप्त होते ही अपील के लिए याचिका दायर की थी और उचित कानूनी सहायता की मदद से खुद ही अपना मामला पेश किया था।
भारत में बहुत से लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, जैसे कि जमानत या अपील का अधिकार, और अगर वे कानूनी सेवाओं का खर्च उठाने में असमर्थ हैं तो कानूनी सहायता कैसे लें, इस बारे में तो उन्हें जानकारी ही नहीं है। यह बात खासकर उन लोगों के लिए सच है जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कम है और जिन्हें जानकारी और सहायता की कमी के कारण कानूनी मामले महंगे और परेशानी भरे लगते हैं।
इसके अलावा, चूँकि समाज में आपराधिक आरोपों वाले या कानूनी मुकदमों में शामिल लोगों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए कई लोग हर कीमत पर कानूनी विवादों से बचना पसंद करते हैं – भले ही इसका मतलब यह हो कि उन्हें किसी चीज़ के अपने अधिकार को छोड़ना पड़े। कई बार, लोग न्याय तक पहुँचने का जोखिम भी नहीं उठा पाते हैं, जिससे वे उसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
वर्तमान मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर विस्तार से चर्चा की है, जिसमें न्याय के लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त करने में मदद करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता के साथ-साथ जनता के बीच इसके बारे में जागरूकता पर जोर दिया गया है। कानून सभी को उनके लिंग, जाति, वर्ग या स्थिति की परवाह किए बिना सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन सुरक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को इन सेवाओं तक पहुँचने के साधनों के बारे में भी पता होना चाहिए।
कानूनी पृष्ठभूमि
भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति के साथ-साथ राज्य के अधिकार और कर्तव्य निहित हैं। संविधान अपने विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से मानव विकास की रक्षा और उत्थान करता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति संविधान में निहित अधिकारों और कर्तव्यों के लिए पात्र है, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रदान किया जाएगा और उल्लंघन होने पर संबोधित किया जाएगा।
ऐसा ही एक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है, जिसे बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संविधान के निर्माण के शुरुआती चरण में मौजूद न होने के बावजूद, मुफ्त कानूनी सहायता अब समाज के विभिन्न वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है।
नि:शुल्क कानूनी सहायता, संक्षेप में, प्राकृतिक न्याय के नियमों को कायम रखते हुए निष्पक्ष और उचित कानूनी प्रक्रिया के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करती है। ऐसी सहायता के बिना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग खुद को विकलांग महसूस करेंगे। आखिरकार, कानूनी सेवाएँ काफी महंगी हैं और अक्सर सभी के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए, निष्पक्ष प्रक्रिया प्रदान करने के लिए जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

जैसा कि पहले मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 19 के साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, जिसके बिना किसी को भी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया किसी भी निष्पक्ष अभियोजन का आधार है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, निःशुल्क कानूनी सहायता आवश्यक है। यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या निःशुल्क कानूनी सहायता केवल गरीबी में रहने वालों को ही प्रदान की जानी चाहिए या इसे इससे आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि ऐसे कैदी जो बाहरी दुनिया से ज़्यादा संवाद करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं।
वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की है, तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के दायरे का विस्तार किया है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 142 के दायरे का यह विस्तार काफी न्यायिक विकास के बाद हुआ है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों सहित समाज के वंचित या हाशिए पर पड़े वर्गों को पूर्ण न्याय दिलाना है। वर्तमान मामले में, कैदियों को भी इसके संरक्षण के दायरे में जोड़ा गया है।
एमएच होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) के तथ्य
इस मामले के याचिकाकर्ता डॉ. होसकोट कर्नाटक विश्वविद्यालय से पीएचडी और एमएससी डिग्री धारक थे, जिनके कार्यों को देखते हुए उन पर भी जालसाजी का आरोप लगाया गया था। पिछले फैसले में याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया गया था और उसे कर्नाटक विश्वविद्यालय के नाम से जाली डिग्री बनाने का दोषी पाया गया था।
याचिकाकर्ता ने कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलपति के निजी सहायक के हस्ताक्षर सहित एक जाली प्राधिकरण पत्र तैयार किया था, जिसके तहत उसे विश्वविद्यालय के नाम वाली आधिकारिक मुहरें बनवाने का अधिकार दिया गया था। इस जाली प्राधिकरण पत्र के साथ याचिकाकर्ता ने बॉम्बे में दाभोलकर नामक एक मुहर-निर्माता से संपर्क किया, जो प्रशासन और शैक्षणिक प्रणालियों के लिए उभरी हुई मुहरें बनाने में विशेषज्ञ था।
एक बार यह उभरी हुई सील प्राप्त हो जाने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा कर्नाटक विश्वविद्यालय के नाम पर डिग्री के नकली प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि, ऐसा होने से पहले ही सील बनाने वाले ने पुलिस को उक्त लेन-देन की सूचना दे दी, जिसके कारण याचिकाकर्ता जालसाजी में रंगे हाथों पकड़ा गया।
सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 417, 467, 468, 471 और 511 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया, जिसके कारण उसे एक दिन के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, न्यायालय ने उसे राज्य द्वारा अपेक्षित की तुलना में बहुत कम सजा सुनाई थी।
इस प्रकार, राज्य और याचिकाकर्ता दोनों ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें एक दिन के कारावास की सजा में संशोधन की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने साधारण कारावास के खिलाफ तर्क दिया, जबकि राज्य ने तर्क दिया कि उपरोक्त धाराओं के तहत ऐसे गंभीर अपराधों के लिए लगाया गया कारावास बहुत हल्का है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए राज्य की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया और कारावास की अवधि को एक दिन से बढ़ाकर तीन साल कर दिया। यह फैसला 22 नवंबर, 1973 को दिया गया, जिसके तीन दिन बाद बॉम्बे के केंद्रीय कारागार प्राधिकरण ने फैसले के अनुरूप याचिकाकर्ता को हिरासत में ले लिया। बाद में, याचिकाकर्ता को पुणे की यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उसे तीन साल की कारावास अवधि के लिए रखा गया।
अपनी रिहाई के बाद याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की, जिसमें चार साल की देरी के बावजूद अपने कारावास से राहत मांगी गई। याचिकाकर्ता ने अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए न्यायालय द्वारा प्रदान की गई पेशेवर कानूनी सहायता की मदद से खुद के लिए बहस करने का विकल्प चुना। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान याचिका दायर करने में देरी बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति के देरी से पहुंचने के कारण हुई, जो उन्हें आवेदन करने के बावजूद कारावास की अवधि पूरी होने तक नहीं मिली।
उठाए गए मुद्दे
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दे इस प्रकार थे:
- क्या वर्तमान याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत स्वीकार्य है?
- क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निःशुल्क कानूनी सहायता की अवधारणा को समाहित करता है।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता
जैसा कि पहले संक्षेप में बताया गया है, याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उसे निर्णय की प्रति प्रदान करने में देरी हुई थी। नवंबर 1973 में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की प्रति याचिकाकर्ता को 1978 में दी गई- इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय द्वारा पुणे के केंद्रीय कारागार के अधीक्षक के माध्यम से इसकी एक निःशुल्क प्रति तुरंत भेजी गई थी, इसमें चार साल से अधिक की देरी हुई।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 10 दिसंबर, 1973 को जेल अधिकारियों के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 363 (2) सहपठित धारा 387 के तहत उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति मांगी थी। हालांकि, याचिकाकर्ता को उनके आवेदन के बावजूद फैसले की कोई प्रति नहीं मिली।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही जेल अधिकारियों को फैसले की प्रमाणित प्रति मिल गई हो, लेकिन तीन साल की कैद के दौरान उसे कभी नहीं दी गई। इसके कारण, याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका के तहत अपील करने का अपना अधिकार खो दिया और 1978 में फैसले की प्रति प्राप्त करने के बाद उसे भारतीय सीमा अधिनियम के तहत क्षमा याचिका का विकल्प चुनना पड़ा।
याचिकाकर्ता का तर्क कि उसे कभी भी फैसले की प्रति नहीं मिली, इस बात से समर्थित था कि इस तरह की डिलीवरी के लिए कोई रिकॉर्ड या रसीद का टोकन नहीं था। चूंकि इसके लिए प्राधिकरण के रजिस्टर में याचिकाकर्ता का कोई हस्ताक्षर नहीं था, इसलिए इस बात का कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता को कभी भी उच्च न्यायालय द्वारा फैसले की प्रति दी गई थी या नहीं।
प्रतिवादी
दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि निर्णय की प्रति प्रदान करने में स्पष्ट विलम्ब उनके अपने कार्यों के कारण नहीं था।
पुणे सेंट्रल जेल के अधीक्षक के अनुसार, उनके कार्यालय के एक क्लर्क ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति दी थी। हालांकि, बाद में याचिकाकर्ता से प्रति वापस ले ली गई क्योंकि इसे सजा की माफी के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल को दया याचिका के साथ संलग्न करना था।
उपर्युक्त पुनर्प्राप्ति के कारण, याचिकाकर्ता को निर्णय की प्रति देने में देरी हुई।
एमएच होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) में चर्चित कानून
वर्तमान मामले के विश्लेषण में चर्चित कानूनी प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
भारत का संविधान, 1949
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भारत के नागरिकों को गारंटीकृत छह मौलिक स्वतंत्रताएँ दी गई हैं:
- वाक् एवं अभिव्यक्ति (स्पीच एंड एक्सप्रेशन) की स्वतंत्रता;
- शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता;
- संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता;
- पूरे भारत में यात्रा करने और घूमने की स्वतंत्रता;
- भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता;
- किसी भी प्रकार का पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
उपर्युक्त अधिकारों पर प्रतिबंध संविधान के उसी अनुच्छेद के शेष खंडों में दिए गए हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है। यह अनुच्छेद कई अन्य अधिकारों के लिए एक छत्र प्रावधान बन गया है जो भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का एकमात्र अपवाद तब है जब किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी भी गैरकानूनी हिरासत या गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों को स्थापित करता है, जिसमें कानूनी पेशेवर से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार, उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार आदि शामिल हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में जरूरतमंद नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और सहायता की राज्य की जिम्मेदारी स्थापित की गई है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क कानूनी सेवाओं के माध्यम से न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य को उचित कानूनी प्रावधान, योजनाएँ आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले या वाद के संबंध में भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी भी फैसले, आदेश, सजा या अन्यथा के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने की शक्ति प्रदान करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी ऐसे आदेश और डिक्री को पारित करने और लागू करने का अधिकार देता है जो उसके समक्ष लंबित मामले या मामले के लिए पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। इसमें अभियोजन के उद्देश्य से किसी भी साक्ष्य, दस्तावेज़, व्यक्ति या अन्य को पेश करने का आदेश शामिल है।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
सीआरपीसी की धारा 304
सीआरपीसी की धारा 304 उन मामलों में कानूनी सहायता से संबंधित है जहां आरोपी कोई कानूनी सेवा प्राप्त करने में असमर्थ है। ऐसे मामलों में, न्यायालय के पास आरोपी के लिए एक प्रतिनिधि अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार है, जिसका खर्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।
सीआरपीसी की धारा 363
सीआरपीसी की धारा 363 में कहा गया है कि न्यायालय के फैसले की प्रमाणित प्रति मामले में शामिल सभी पक्षों को दी जानी चाहिए, खासकर अभियुक्तों को जब उनके खिलाफ कोई सजा सुनाई जाती है। इस धारा के तहत, फैसले की प्रति का अनुरोध करने के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है, चाहे वह न्यायालय की भाषा में हो या किसी अन्य भाषा में जिसे आवेदक सहज महसूस करता हो। वितरण निःशुल्क और तत्काल होना चाहिए, खासकर मृत्युदंड या अन्य गंभीर दंड के मामलों में।
इस धारा के तहत, आवेदक किसी भी आपराधिक न्यायालय के आदेशों या फैसलों की प्रतियों का अनुरोध कर सकता है, भले ही वह मामले में पक्षकार न हो, लेकिन यदि उच्च न्यायालय इसकी अनुमति देता है तो वह निर्धारित शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो इसके लिए शुल्क माफ किया जा सकता है।
सीआरपीसी की धारा 387
सीआरपीसी की धारा 387 के अनुसार, सीआरपीसी के अध्याय XXVII में वर्णित सभी नियम, जो मूल अधिकार क्षेत्र के आपराधिक न्यायालयों पर लागू होते हैं, वे अपीलीय न्यायालयों जैसे सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर भी लागू होंगे।

भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी की धारा 417
भारतीय दंड संहिता की धारा 417 धोखाधड़ी के लिए दंड से संबंधित है, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
आईपीसी की धारा 467
आईपीसी की यह धारा सुरक्षा, वसीयत, अधिकार पत्र या किसी भी ऐसे दस्तावेज़ की जालसाजी से संबंधित है जो किसी अन्य व्यक्ति को किसी मूल्यवान वस्तु का अधिकार देता है। इस धारा के तहत, जालसाजी का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को दस साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। मामले की गंभीरता के आधार पर, सजा को आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 468
आईपीसी की धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी के अपराध से संबंधित है। इस धारा के अनुसार, उक्त अपराध का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सात साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह धारा किसी दस्तावेज़ की भौतिक और डिजिटल दोनों प्रतियों की जालसाजी के लिए लागू होती है।
आईपीसी की धारा 471
धारा 471 किसी जाली दस्तावेज़ का उपयोग करने से संबंधित है, चाहे वह भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रति हो, यह जानते हुए भी कि वह असली नहीं है, उसे असली के रूप में इस्तेमाल करना। इस धारा के तहत, ऐसा करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को धारा 467 के तहत दी गई सजा के समान ही दंडित किया जाएगा, जैसे कि उसने स्वयं ही दस्तावेजों को जाली बनाया हो।
आईपीसी की धारा 511
आईपीसी की धारा 511 एक सामान्य प्रावधान है जो किसी अपराध के प्रयास के लिए सजा से संबंधित है। सरल शब्दों में, भले ही आरोपी योजना के अनुसार आपराधिक अपराध करने में सफल न हुआ हो, लेकिन ऐसा करने का उसका प्रयास भी उसी तरह गिना जाएगा। इस धारा के तहत, जिस व्यक्ति ने आईपीसी के तहत अपराध करने का प्रयास किया था, उसे उसी तरह की सजा दी जाएगी जैसे कि अगर वह अपराध करने में सफल रहा होता।
एमएच होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) में निर्णय
निर्णय के पीछे का तर्क
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें वे सभी पहलू शामिल हैं जो इसे प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति को उसके समग्र विकास या अपनी इच्छानुसार जीवन जीने से वंचित कर सकती है, उसे इस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एक तरह से, यह अनुच्छेद संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के दायरे में शामिल किए जाने वाले अन्य मानवाधिकारों के लिए एक छत्र के रूप में खड़ा है।
अनुच्छेद 21 का एकमात्र अपवाद तब है जब जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, केवल भारतीय कानूनों के भीतर स्थापित निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के तहत अधिकारों से वंचित किया जा सकता है।
‘निष्पक्ष और उचित’ प्रक्रिया, जो प्राकृतिक न्याय में निहित है, में उस न्यायाधिकरण से उच्चतर पीठ में अपील करने का अधिकार भी शामिल है, जिसमें मामले की सुनवाई हुई थी। यह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों के लिए लागू है, जैसे कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने पिछले आपराधिक अभियोजन के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
अपील निष्पक्ष प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय का एक अभिन्न अंग है, जो मामले के दोनों पक्षों को सुनवाई और सुनवाई के लिए उचित समय और चरण प्रदान करता है। अपील का हर चरण महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ अनिवार्य भी है और इसमें कोई भी निष्क्रियता या बाधा अन्याय और पक्ष के अधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकती है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है।
वर्तमान मामले के निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अपील के अधिकार में प्रत्येक कदम निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है और यदि किसी अन्य की कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण ऐसा कोई भी कदम बाधित होता है, तो यह अनुचित होगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के साथ अनुच्छेद 21 के तहत निहित अधिकारों का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि मेनका गांधी मामले में यह दृष्टिकोण पहले कैसे स्थापित किया गया था, जहां यह निर्धारित किया गया था कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के बिना, किसी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 39A के तहत नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच का एक आवश्यक हिस्सा है। चूंकि कानूनी फीस काफी अधिक हो सकती है और कई लोगों के लिए अक्सर वहनीय नहीं होती है, इसलिए राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क कानूनी सहायता का विकल्प चुनने से ऐसी पृष्ठभूमि के लोगों को अक्सर पेशेवर कानूनी सेवा के अभाव में होने वाली विकलांगता की भावना से बचा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां
सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में दो प्रमुख बिंदुओं पर गौर किया; पहला यह कि अभियुक्त या कैदी को आगे की अपील के लिए सीमा अवधि के भीतर फैसले की प्रमाणित प्रति प्रदान की जाए और दूसरा यह कि ऐसे व्यक्तियों, विशेष रूप से कैदियों के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाओं का प्रावधान किया जाए, जो अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण पेशेवर कानूनी सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ये दोनों बिंदु राज्य की ज़िम्मेदारियों के अंतर्गत आते हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत और जहाँ भी प्रक्रियात्मक कानून प्रदान करते हैं, वहाँ लागू होते हैं, जिसमें उच्च पीठ के समक्ष आगे की अपील भी शामिल है।
वर्तमान मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले की प्रति देने में देरी के कारण याचिकाकर्ता का अपील करने का अधिकार समाप्त हो गया। राज्य की ओर से इस निष्क्रियता के कारण, जिस पर कैदी को आदेश या फैसले की प्रति देने की जिम्मेदारी है, याचिकाकर्ता अपील करने में सक्षम नहीं था और ऐसा करने से पहले उसे अपने कारावास की अवधि पूरी होने तक इंतजार करना पड़ा।
कैदी को आदेश या निर्णय की उचित सेवा न मिलने से कैदी के अपील करने के अधिकार का उल्लंघन होता है, साथ ही अगर बिना सुधार के ऐसा जारी रखा जाता है तो अवैध या गैरकानूनी हिरासत का रास्ता भी प्रशस्त होता है। सिर्फ़ इसलिए कि किसी व्यक्ति को कैद कर लिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि उससे उसके संवैधानिक और वैधानिक अधिकार छीन लिए गए हैं, जिसमें अपील और विशेष अनुमति याचिकाएँ शामिल हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो, यह सुनिश्चित करने में कानूनी सहायता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे उनकी स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के साथ अनुच्छेद 39A और 21 न्यायालय को उन अभियुक्त पक्षों के लिए सक्षम वकील नियुक्त करने का अधिकार देते हैं जो जेल में बंद हैं, खासकर तब जब वे अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण कानूनी सेवाएँ प्राप्त करने में असमर्थ हों।
यह भी देखा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) में भी कानूनी व्यवसायी का उल्लेख है, लेकिन इसका दायरा बहुत अधिक सामान्य है। इस प्रकार, जेल स्थितियों में कानूनी सहायता के उद्देश्य से अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 39ए के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
उपर्युक्त तर्कों और टिप्पणियों के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फैसला सुनाए जाने में हुई देरी को माफ कर दिया, लेकिन फिर भी मौजूदा याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने पक्षकारों को फैसले की एक प्रति देने के साथ-साथ कानूनी सेवाएं हासिल करने में असमर्थ लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के संबंध में कुछ नियम स्थापित किए।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामले के सभी पक्षों को न्यायालय द्वारा पारित आदेश या निर्णय की प्रति प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वह दीवानी मामला हो या आपराधिक। खासकर ऐसे मामलों में जहां अभियुक्त को कारावास की सजा सुनाई गई हो, अभियुक्त को उसी सजा वाले फैसले की प्रमाणित प्रति मांगने का अधिकार है।
यदि अभियुक्त पहले से ही जेल में है, तो न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति की सेवा जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसी डिलीवरी बिना किसी अनावश्यक देरी के और अपील दायर करने की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अभियुक्त तक पहुँच जाए, इसके लिए ऐसी डिलीवरी की लिखित पावती भी प्राप्त की जानी चाहिए।
न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां कैदी अपने मामले में संशोधन या अपील दायर करना चाहता है, जेल अधिकारियों को कैदी को उसके प्रयास में मदद करने के लिए हर सुविधा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह के कदम के दौरान कोई भी बाधा गंभीर अन्याय को जन्म देगी, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है।
यह भी माना गया कि कोई भी जेलर या जेल अधिकारी कैदियों को आधिकारिक अदालती दस्तावेजों की प्रतियों की डिलीवरी को रोकता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 363 और संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की हरकतें निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया में बाधा बनती हैं और कैदी की गैरकानूनी या अवैध हिरासत का कारण बन सकती हैं।
न्यायालय ने वर्तमान निर्णय में निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता पर भी विस्तार से चर्चा की, जिसमें कहा गया कि न्यायालय का यह दायित्व है कि वह कैदी के लिए सक्षम वकील नियुक्त करे, ऐसे मामलों में जहां कैदी खराब आर्थिक पृष्ठभूमि या बाहर किसी से संवाद की कमी के कारण पेशेवर कानूनी सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ है, खासकर ऐसे मामलों में जहां अपराध की गंभीरता और उसके बाद की सजा गंभीर है और कैदी के लिए उचित वकील नियुक्त किए बिना गंभीर अन्याय हो सकता है। कैदी ऐसे किसी वकील या नियुक्त किए गए विशेष वकील पर भी आपत्ति कर सकता है।
नियुक्त वकील की कानूनी फीस उस राज्य द्वारा अदा की जाएगी जिसने अभियुक्त पर मुकदमा चलाया था, जिसे उस न्यायालय द्वारा न्यायसंगत रूप से तय किया जाएगा जहां मामला चल रहा है।
निर्णय का विश्लेषण
वर्तमान निर्णय उन मिसालों में से एक है जिसने भारत में मुफ्त कानूनी सहायता की मौजूदगी को और अधिक प्रमुख बना दिया है, खासकर जेल में बंद लोगों के लिए। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, जेल में बंद लोगों के खिलाफ़ बहुत सारे कलंक हैं – भले ही कोई अपने सभी आरोपों से बरी हो जाए, फिर भी कानूनी मुद्दों में उलझने और आपराधिक आरोपों का सामना करने के कारण उन्हें बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इस पूर्वाग्रह के अलावा, ज़्यादातर कैदियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। कई कैदियों को जेल में बंद कर दिया जाता है और कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ कैदियों के बुनियादी मानवाधिकारों का भयानक उल्लंघन किया गया है।
ऐसी परिस्थितियों में, कैदियों के लिए न्याय तक पहुँच काफी कठिन हो जाती है, खासकर तब जब उनमें से अधिकांश बाहरी दुनिया से काफी कटे हुए होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि जेल से अपने लिए कानूनी सेवाएँ कैसे प्राप्त करें। जेल में बंद होना और अपने अपराधों के लिए दोषी पाया जाना किसी व्यक्ति की स्थिति को एक व्यक्ति से गैर-व्यक्ति में गिराने के बराबर नहीं है।

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जेल में बंद लोगों के लिए न्याय दर में भारी सुधार हुआ, विशेष रूप से अपील करने और अपने सजा के फैसले की एक प्रति के लिए अनुरोध करने के उनके अधिकार के संदर्भ में। इसके अलावा, मुफ्त कानूनी सहायता के दायरे के संबंध में दिए गए विस्तृत विचार-विमर्श और दिशा-निर्देशों ने भी अवधारणा के आगे विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, जो भारत जैसे देश के लिए काफी आवश्यक है, जहां कई लोग न्याय चाहते हैं, लेकिन कानूनी सेवाओं का खर्च वहन नहीं कर सकते। वर्तमान समय के विपरीत, उस समय मुफ्त कानूनी सेवाओं और सहायता के बारे में जागरूकता उतनी प्रचलित नहीं थी और इस मामले ने जरूरतमंदों के लिए उन्हें और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक मिसाल कायम की।
याचिका खारिज होने के बावजूद, प्रक्रियात्मक और कानूनी देरी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश कैदियों के अधिकारों के न्यायिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा, वर्तमान निर्णय में कैदियों को संबंधित मामलों के कानूनी दस्तावेज और प्रतिलेख वितरित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए, जो कि कैदियों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। राज्य को उनकी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराना भी ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति (रिक्योरेंस) को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम था।
निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए एक व्यापक दायरे की व्याख्या करने के साथ-साथ उनके प्रतिनिधित्व के लिए एक सक्षम वकील नियुक्त करने के लिए अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 142 के साथ आगे विस्तारित करना इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने न्यायिक प्रणाली को उस रूप में आकार दिया जैसा कि हम वर्तमान में जानते हैं।
एमएच होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) का महत्व
वर्तमान निर्णय न्याय प्रणाली से संबंधित कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से कैदियों के साथ व्यवहार और किस तरह से कैदियों के अधिकारों का हमेशा सबसे पहले हनन किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कैदियों के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक पूर्वाग्रह है और यह व्यक्ति द्वारा अपनी सजा पूरी करने के दौरान और उसके बाद भी जारी रहता है।
इस तरह के पूर्वाग्रह खास तौर पर उन मामलों में देखे जाते हैं जहां कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है। याचिकाकर्ता को समय सीमा के भीतर अपील करने के उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया क्योंकि देरी को उचित रूप से साबित नहीं किया जा सका। यह लापरवाही का परिणाम था, जिसे कैदियों से संबंधित मामलों में बार-बार देखा जा सकता है। इस तरह की लापरवाही से न केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, बल्कि कैदियों के जीवन के कई साल बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है।
वर्तमान निर्णय में इस संबंध में प्रक्रियागत और कानूनी देरी को भी संबोधित किया गया, साथ ही कैदियों के मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकारों को भी शामिल किया गया। इसके कारण इस मामले को कैदियों के अधिकारों के विकास के साथ-साथ जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में उद्धृत किया गया, चाहे वे गरीबी से पीड़ित हों या वे जो जेल में रहने जैसी परिस्थितियों के कारण कानूनी सेवाएं हासिल करने में असमर्थ हैं।
यह निर्णय कैदी के अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला निर्णय था, जिसके दृष्टिकोण को बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) जैसे कई अन्य ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा समर्थित किया गया। इस मामले में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा गया, जिसने स्थापित किया कि निष्पक्ष कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाएँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा हैं, जिसके बिना किसी को भी उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
वर्तमान मामले और मुफ़्त कानूनी सहायता के बारे में इसके दृष्टिकोण का हवाला देते हुए एक और ऐतिहासिक निर्णय हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1979) था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि मुफ़्त कानूनी सहायता किसी भी आरोपी पक्ष के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे उन्होंने कोई भी अपराध किया हो। इसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानूनी सहायता के अधिकार और विचाराधीन कैदियों के लिए उनके अधिकारों के आगे उल्लंघन से बचने के लिए त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर भी चर्चा की।
खत्री बनाम बिहार राज्य (1980) में भी वर्तमान निर्णय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया गया, जहाँ न्यायालय ने माना कि राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह ऐसे अभियुक्त पक्ष को कानूनी सहायता और सहायता प्रदान करे जो पेशेवर कानूनी सेवाओं का खर्च उठाने या उन्हें पाने में असमर्थ है। इसने स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका और ऐसा करना उनका दायित्व कैसे है, इस पर भी चर्चा की।
इन मामलों के अलावा, प्रक्रियात्मक और कानूनी देरी को कम करने के लिए और भी विकास किए गए हैं, जैसे कि हाल ही में ‘फास्टर 2.0‘ नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है, जो कैदियों की सजा और रिहाई के आधिकारिक न्यायालय के आदेशों और फैसलों को सूचीबद्ध करता है। यह पोर्टल भारत भर के सभी जेल अधिकारियों के लिए उपलब्ध और आसानी से सुलभ है, जिसका उद्देश्य बिना किसी भ्रम या देरी के तत्काल सूचना देना है। पोर्टल से न्यायालय के फैसले या आदेश की प्रति को प्रिंट करके कैदियों के साथ साझा किया जा सकता है ताकि किसी भी अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
इसके अलावा, न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर निःशुल्क कानूनी सहायता और सहायता को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 जैसे कानून द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या नालसा जैसे वैधानिक प्राधिकरण भी स्थापित किए गए थे। 2016 में, मॉडल जेल मैनुअल पेश किया गया था, जिसमें कैद व्यक्तियों द्वारा चुनी जा सकने वाली कानूनी सेवाओं और सहायता के बारे में और दिशा-निर्देश और जानकारी दी गई थी।
जेलों की स्थिति सुधारने के लिए 2000 के दशक की शुरुआत में जेलों के आधुनिकीकरण योजना जैसी राष्ट्रव्यापी योजनाएँ भी शुरू की गईं, जिसे बाद में 2021 में जेलों के आधुनिकीकरण परियोजना में बदल दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में कई जेलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कैदियों की रहने की स्थिति में सुधार करना और कैदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करना है। सरकार द्वारा जेल सुरक्षा प्रणालियों को समय के साथ डिजिटल बनाने के लिए ई-जेल परियोजना जैसी अन्य परियोजनाएँ भी शुरू की गईं।

निष्कर्ष
अंत में, एमएच होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले ने भारत में कैदियों के अधिकारों के लिए एक मिसाल कायम की, जिसमें कैदियों द्वारा सामना किए जाने वाले उल्लंघन और ऐसी परिस्थितियों में कानूनी सहायता की आवश्यकता को मान्यता दी गई। जबकि याचिका को खारिज कर दिया गया था, न्यायिक अधिकारियों द्वारा कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और कानूनी दस्तावेजों की वितरण के बारे में दिशानिर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
इस निर्णय में प्रक्रियागत और कानूनी देरी के नकारात्मक परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया, खास तौर पर अपील के अधिकार जैसे अधिकारों के संबंध में, जिनकी समय-सीमा कम होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों के कर्तव्यों पर विस्तार से चर्चा की, साथ ही अपील या पुनरीक्षण के लिए कैदियों को आवश्यक किसी भी और सभी कानूनी सहायता प्रदान करने के उनके दायित्व पर भी चर्चा की।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
एक कैदी के मूल अधिकार क्या हैं?
भारत में, कैदियों को किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपने सभी बुनियादी मानवाधिकारों को बरकरार रखना पड़ता है, सिवाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिबंध के, जो उचित प्रक्रिया के साथ स्थापित किए गए हैं। इन अधिकारों में कानूनी पेशेवर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार, सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का अधिकार, अपनी जमानत और अदालत के फ़ैसलों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार आदि शामिल हैं। इनमें से अधिकांश अधिकार संविधान के साथ-साथ कैदी अधिनियम, 1894 जैसे अन्य वैधानिक प्रावधानों में निहित हैं।
क्या कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता मिल सकती है?
हां, कैदियों को भी संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाता है। जो व्यक्ति अपनी खराब आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण या बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे होने के कारण कानूनी सेवाएं प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वे राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता का विकल्प चुन सकते हैं।
क्या निःशुल्क कानूनी सहायता मौलिक अधिकारों का हिस्सा है?
हां, निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अनुच्छेद 39A के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का भी हिस्सा है।
संदर्भ
- M. Seervai, Constitutional Law of India, Universal Law Publishing Co., Reprint 2013.
- M. Bakshi, The Constitution of India, Universal Law Publishing Co., 2014.
- Dr J.N. Pandey, Constitutional Law of India, Central Law Agency, Allahabad, 37th edition, 2001.