यह लेख Shweta Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय का विस्तृत विश्लेषण तथा उसके पीछे के तर्क दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें मामले के विस्तृत तथ्य और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क भी शामिल हैं, ताकि मामले के निर्णय के मुद्दे पर निहितार्थ (इंप्लीकेशंस) को बेहतर ढंग से समझा जा सके। प्रिवी काउंसिल द्वारा तय किया गया मुख्य मुद्दा यह था कि हिंदुओं पर लागू कानूनों के तहत पैतृक संपत्ति क्या है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
मुहम्मद हुसैन खान बनाम बाबू किश्व नंदन सहाय (1937) मामले का निर्णय 7 मई, 1937 को हुआ, जब प्रतिवादियों ने प्रिवी काउंसिल में अपील करने का निर्णय लिया। यह मामला हिंदू कानून के तहत पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून से संबंधित था। विशेष रूप से, इसमें पैतृक पक्ष से प्राप्त संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित नियमों का विश्लेषण किया गया। हिंदुओं पर लागू उत्तराधिकार से संबंधित कानून में यह प्रावधान है कि पिता, दादा और परदादा सहित परिवार के पिता की ओर से विरासत में मिली कोई भी संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है और पुत्र को वंशज माना जाता है। यह मामला मुख्य रूप से हिंदू समुदाय में उत्तराधिकार कानून की मिताक्षरा पद्धति से संबंधित था। यह लेख दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों और प्रासंगिक कानूनों और उदाहरणों के प्रकाश में प्रिवी काउंसिल के निर्णयों की जांच करता है।
मामले के तथ्य
गणेश प्रसाद आगरा प्रांत के बांदा के निवासी थे और विवादित गांव सहित एक बड़ी और मूल्यवान संपत्ति के मालिक थे। 10 मई, 1914 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद, उनके जीवित पुत्र बिन्देश्री प्रसाद को राजस्व अभिलेखों में संपत्ति के मालिक के रूप में आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया। बिन्देश्री प्रसाद के विरूद्ध ऋणदाताओं द्वारा धन वसूली हेतु जारी डिक्री के निष्पादन (एक्जिक्यूशन) में कालिंजर तिरहटी गांव को बिक्री के लिए रखा गया तथा उसे 20 नवम्बर, 1924 को बेच दिया गया, यद्यपि बिक्री की पुष्टि 25 जनवरी, 1925 को हुई।

इससे व्यथित होकर बिंदेश्री प्रसाद ने इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि बिक्री धोखाधड़ी से हुई थी। 25 दिसम्बर, 1926 को उनका निधन हो गया और मार्च, 1927 में प्रतिवादी गिरि बाला ने अपने दिवंगत पति के स्थान पर वादी बनने के लिए आवेदन किया। अनुरोध स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि वह उनकी संपत्ति की एकमात्र लाभार्थी थी। उन्होंने शिकायत में संशोधन के लिए भी आवेदन किया, जिसमें कहा गया कि 5 मई 1914 को उनके ससुर गणेश प्रसाद द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार, वह विवादित गांव की हकदार थीं। उनके पति को संपत्ति में आजीवन अधिकार प्राप्त था और इसलिए, उनकी मृत्यु के बाद, वह संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन गईं। उन्होंने कहा कि हालांकि यह बिक्री उनके पति के विरुद्ध है, लेकिन इससे उनके स्वामित्व अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
परीक्षण न्यायाधीश ने 28 मई, 1927 को संशोधन को अनुमति दे दी, जिस पर प्रतिवादी (वर्तमान मामले में अपीलकर्ता) ने आपत्ति की और इसके कारण न्यायाधीश को उक्त संशोधन की वैधता से संबंधित मुद्दा तैयार करना पड़ा। बाद में न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया, तथा नये न्यायाधीश ने कई आधारों पर मुकदमे को खारिज कर दिया, जिनमें से एक यह था कि संशोधन ने मुकदमे की प्रकृति को बदल दिया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा की गई अपील में इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि पक्षों के बीच मामले में वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संशोधन आवश्यक था। वर्तमान मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 23 जनवरी, 1933 के आदेश के विरुद्ध अपील था, जिसमें बांदा के अधीनस्थ न्यायाधीश के 17 जनवरी, 1929 के आदेश को पलट दिया गया था और वादी के कालिंजर तिरहटी गांव पर कब्जे के दावे को मध्यवर्ती लाभ (मेसने प्रॉफिट) सहित स्वीकार कर लिया गया था।
1914 की वसीयत के निष्पादन (एक्जिक्यूशन) से जुड़े तथ्य
वसीयत के अस्तित्व से संबंधित प्रासंगिक मुद्दे को समझने के उद्देश्य से, उन तथ्यों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जो अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित वसीयत के अस्तित्व को साबित करते हैं। वसीयत के निष्पादन से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:
- 1898 में गणेश प्रसाद ने अपनी संपत्ति का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए अपने प्रांत की सरकार से आवेदन किया। अपने जीवन के अंतिम चार वर्षों में उन्होंने अपनी संपत्ति पर कब्ज़ा पुनः पाने के लिए कई बार प्रयास किये, लेकिन उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली।
- गणेश प्रसाद का एक बेटा था, बिन्देश्री प्रसाद, जिसके साथ उसके अनुचित चरित्र और फिजूलखर्ची की प्रवृत्ति के कारण उनके संबंध तनावपूर्ण थे। इसलिए, 4 अगस्त 1911 को गणेश प्रसाद ने इलाहाबाद में वसीयत बनाई और अगले दिन उसका पंजीकरण भी करा लिया। वसीयत के अनुसार, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान कर दी और न्यास (ट्रस्ट) के लिए सात निष्पादकों और न्यासियों (ट्रस्टी) को नामित किया। इन निष्पादकों में श्री स्वान भी शामिल थे, जो बांदा जिले के कलेक्टर थे और उस समय भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। श्री स्वान को गणेश प्रसाद से वसीयत की एक प्रति प्राप्त हुई थी और इसलिए वे वसीयत के निष्पादन और विषय-वस्तु से अवगत थे।
- इस वसीयत के द्वारा गणेश प्रसाद ने न केवल अपने बेटे बिंदेशरी प्रसाद को विरासत से वंचित कर दिया, बल्कि अपनी बहू गिरि बाला या भविष्य में उससे पैदा होने वाले किसी भी बच्चे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया।
- 1914 में बांदा में प्लेग फैलने के दौरान गणेश प्रसाद बीमार पड़ गये और मोतिहारी चले गये। वहां रहते हुए उन्होंने 5 अप्रैल, 1914 को 1911 की वसीयत को निरस्त करते हुए एक नई वसीयत बनाई। वे बांदा लौट आये और 10 मई 1914 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद, श्री स्वान ने उनकी मूल्यवान वस्तुओं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उनकी सुरक्षा के लिए अपने कब्जे में ले लिया। श्री स्वान के निर्देशानुसार, उप कलेक्टर पंडित राम अधीन शुक्ला ने मृतक के कमरे की कुंडी लगा दी, जिसमें उसकी मृत्यु के दिन दोपहर में कई बंद बक्से और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। अगले दिन शुक्ला ने एक लिखित रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंप दी।
- 1911 में पहले से निष्पादित वसीयत के न्यासियों को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि इसे रद्द कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने 3 जून 1914 को प्रोबेट के लिए आवेदन दायर किया, यह सोचकर कि यह वसीयत उनके निधन के बाद लागू हुई। न्यासियों ने 1911 में बनाई गई वसीयत की प्रमाणित प्रति जमा कर दी और दावा किया कि मूल प्रति गणेश प्रसाद के दस्तावेजों में मिल सकती है।
- उच्च न्यायालय ने बांदा के कलेक्टर को 1911 में बनी मूल वसीयत पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन उप कलेक्टर को 1914 में बनी वसीयत मिली। कलेक्टर गणेश प्रसाद की लिखावट जानते थे और इसलिए उनके पास वसीयत की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था और इसलिए उन्होंने इसकी सूचना उच्च न्यायालय को दे दी। उन्होंने सरकारी वकील को 1911 की वसीयत के प्रोबेट को चुनौती देने और 1914 की वसीयत को अदालत में पेश करने का आदेश दिया। बांदा के कलेक्टर के निर्देशानुसार, 27 जुलाई 1914 को प्रोबेट कार्यवाही के दौरान सरकारी वकील द्वारा मूल वसीयत उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इसके बाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले में अगले आदेश तक वसीयत को रजिस्ट्रार की हिरासत में रखा जाए।
- इस बीच, बिंदेश्री प्रसाद ने 1911 की वसीयत के प्रोबेट को चुनौती दी और पैतृक अधिकारों का दावा करते हुए संपत्ति के नामान्तरण (म्यूटेशन) की मांग की।
- बिन्देश्री प्रसाद और 1911 की वसीयत के न्यासियों के बीच दाखिल खारिज की कार्यवाही में 5 अक्टूबर 1914 को समझौता हुआ। इन न्यासियों ने पुष्टि की कि 1914 में निष्पादित वसीयत वास्तविक थी और उस पर गणेश प्रसाद ने हस्ताक्षर किये थे। वे 1914 की वसीयत के अनुसार बिंदेश्री प्रसाद को अपने पिता की संपत्ति का स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति देने पर सहमत हुए। वे उच्च न्यायालय में जाकर 1911 की वसीयत के उनके प्रोबेट आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करने पर भी सहमत हो गए। बदले में, बिंदेशरी प्रसाद ने अपने पिता के बकाया ऋण का भुगतान करने, संपत्ति में एक घर के लिए एक न्यास स्थापित करने, जिसका उपयोग धर्मशाला के रूप में किया जाएगा, और बांदा में रामलीला के प्रदर्शन के खर्च के लिए प्रति वर्ष 300 रुपये का योगदान देने का वादा किया।
- 7 नवंबर, 1914 को उच्च न्यायालय ने प्रोबेट आवेदन खारिज कर दिया और उसी वर्ष दिसंबर में राजस्व (रेवेन्यू) अधिकारी ने बिंदेशरी प्रसाद के पक्ष में संपत्ति के नामान्तरण को मंजूरी दे दी। हालाँकि, कार्यवाही के बाद 1914 की मूल वसीयत खो गई, और खोज के बावजूद भी उसे बरामद नहीं किया जा सका।
मामले में उठाए गए मुद्दे
मामले में उठाए गए प्रासंगिक मुद्दे इस प्रकार हैं:
- क्या उच्च न्यायालय के फैसले को केवल गलत संयोजन के आधार पर पलट दिया जाना चाहिए?
- क्या 1914 में बनाई गई वसीयत वैध और वास्तविक थी?
- क्या गिरि बाला का विवादित गांव पर वैध अधिकार था?
- क्या वसीयत के तहत दी गई संपत्ति पैतृक है और क्या गणेश प्रसाद के बेटे का उसमें उनके साथ संयुक्त हित है?
मामले में पक्षकारों की दलीलें
दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावों के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किए। इस मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए फैसले को समझने के लिए, सबसे पहले अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गौर करना महत्वपूर्ण है।
अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क
प्रतिवादियों, जो इस मामले में अपीलकर्ता थे, ने तर्क दिया कि बिंदेशरी प्रसाद की विधवा के रूप में गिरि बाला, अपने पति द्वारा उनकी मृत्यु से पहले स्थापित किए गए वाद के तहत मुकदमा जारी रख सकती हैं। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि गिरि बाला को एक नया, अलग और पूरी तरह से स्वतंत्र मामला लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत अधिकारों और क्षमता से उत्पन्न हुआ हो। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि यद्यपि वह अपने पति द्वारा शुरू किए गए दावे को आगे बढ़ाना जारी रख सकती थी, लेकिन उसने गणेश प्रसाद की वसीयत के आधार पर कब्जे के लिए अपने व्यक्तिगत दावे को शामिल करने के लिए शिकायत में संशोधन करने की मांग करके अपनी कानूनी सीमाओं का अतिक्रमण किया, जो उसके पति द्वारा मांगी गई मूल राहत का हिस्सा नहीं था। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनका दावा, जो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से किया था, अनुचित था और उनके पति के मुकदमे को जारी रखने के संबंध में उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि 1914 की वसीयत के तहत दी गई संपत्ति पैतृक संपत्ति थी और इसलिए गणेश प्रसाद को उसका निपटान करने का कोई अधिकार नहीं था। परिणामस्वरूप, 1914 में बनाई गई वसीयत को अवैध माना जाना चाहिए।
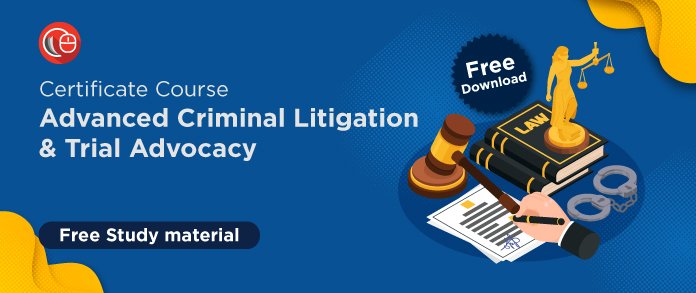
प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए तर्क
दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने संशोधन को अनुमति दी, जिससे कार्रवाई का एक अतिरिक्त कारण सामने आया, और इस तरह के निर्णय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे सी.पी.सी. कहा जाएगा) की धारा 99 के अनुसार उलटा या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विचाराधीन कार्रवाई के कारण के गलत संयोजन से मामले की योग्यता या अधिकारिता प्रभावित नहीं होती। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि मुकदमा संशोधित शिकायत के आधार पर चलाया गया था, जिसमें कार्रवाई के मूल और नए दोनों कारण शामिल थे। आगे यह भी बताया गया कि दोनों पक्षों ने दोनों कारणों के संबंध में सभी आवश्यक साक्ष्य पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह तर्क दिया गया कि वाद में संशोधन के संबंध में आपत्ति के कारण, मुकदमे पर खर्च किए गए समस्त समय और प्रयास की उपेक्षा करना अनुचित होगा।
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य तर्क यह था कि विवादित संपत्ति, जो 1914 में की गई वसीयत का विषय है, “पैतृक संपत्ति” की श्रेणी में नहीं आती है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कई न्यायालयीन निर्णयों का हवाला दिया कि केवल वही संपत्तियां पैतृक मानी जा सकती हैं जो पिता या पैतृक वंश में अन्य पुरुष संबंधियों से विरासत में मिली हों, जैसा कि मूल मिताक्षरा ग्रन्थ में प्रावधान है। संदर्भित मामले करुप्पई नाचियार बनाम शंकरनारायणन चेट्टी (1903), बिश्वमथ प्रसाद साहू बनाम गंजधर प्रसाद (1917) और राजा चेलिकानी वेंकैयाम्मा गारू बनाम राजा चेलिकानी वेंकटरामनय्याम्मा (1902) थे। इसलिए, चूंकि विचाराधीन संपत्ति गणेश प्रसाद को उनके नाना से प्राप्त हुई थी, इसलिए इसे पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, उनके पास अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत के माध्यम से ऐसी संपत्ति का निपटान करने की पूरी क्षमता थी।
मामले का निर्णय
प्रिवी काउंसिल ने माना कि अतिरिक्त कारण के आधार पर चलाया गया मुकदमा कानूनी था और उच्च न्यायालय द्वारा वाद में संशोधन की अनुमति देकर तथा नया कारण शामिल करके सही निर्णय लिया गया। आगे यह भी माना गया कि चूंकि गणेश प्रसाद को विरासत में जो संपत्ति मिली थी, वह उनके नाना से मिली थी, इसलिए ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति है जिसमें पुत्र को जन्म से ही अपने पिता के साथ हिस्सा प्राप्त होता है, तथा केवल वही संपत्ति पैतृक मानी जा सकती है जो पिता या पैतृक वंश में अन्य पुरुष संबंधियों से विरासत में प्राप्त होती है, जैसा कि मूल मिताक्षरा ग्रन्थ में प्रावधान है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि गणेश प्रसाद को संपत्ति का निपटान करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्रवधू गिरि बाला के पक्ष में जो वसीयत तैयार की है, उस पर उनका बेटा या कोई अन्य व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता। जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उनकी अंतिम वसीयत की शर्तें लागू हो गईं और कालिंजर तिरहटी गांव तथा संपूर्ण संपत्ति के संबंध में सभी स्वामित्व अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए। उस गांव की बिक्री से, उसके पति के खिलाफ निष्पादन की कार्यवाही में, उसके हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन कारणों से, उनके माननीय न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की तथा इस अपील को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। इस मामले में पारित निर्णय को समझने के लिए प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए विस्तृत मुद्देवार निर्णय पर गौर करना उचित होगा।
निर्णय के पीछे के तर्क
क्या उच्च न्यायालय के फैसले को केवल गलत संयोजन के आधार पर पलट दिया जाना चाहिए
माननीय न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि गिरि बाला अपने दिवंगत पति के वाद के आधार पर मामले को निष्कर्ष तक ले जा सकती थीं, लेकिन वह अपने अधिकारों के आधार पर स्वतंत्र वाद का कारण नहीं बना सकती थीं। उन्होंने इस तर्क को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मुकदमा संशोधित शिकायत के आधार पर किया गया था, जिसमें कार्रवाई के मूल और नए कारण दोनों शामिल थे। यह भी उल्लेख किया गया कि दोनों पक्षों ने कार्रवाई के दोनों कारणों के संबंध में सभी आवश्यक साक्ष्य पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं। मामले के ऐसे तथ्यों पर भरोसा करके, उनके माननीय न्यायाधीशों ने निष्कर्ष निकाला कि वाद में संशोधन के संबंध में आपत्ति के कारण, मुकदमे पर खर्च किए गए सभी समय और प्रयास की उपेक्षा करना अन्यायपूर्ण होगा। सी.पी.सी. की धारा 99 का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि पक्षकारों के गलत संयोजन या कार्रवाई के कारणों या प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य अनियमितता के कारण, जो न्यायालय के गुण-दोष या अधिकारिता को प्रभावित नहीं करती है, किसी भी डिक्री को उलटा नहीं किया जाएगा या उसमें पर्याप्त परिवर्तन नहीं किया जाएगा या किसी मामले को अपील में वापस नहीं भेजा जाएगा।
आगे यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में माना था कि दोनों कारणों से मुकदमे की सुनवाई कानूनी थी, और यह भी देखा गया कि विचाराधीन गलत संयोजन से मामले की योग्यता या अधिकारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार, जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना बाकी था, वह यह था कि क्या पक्षों के गलत संयोजन के कारण उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर निर्णय करते समय, उनके माननीय न्यायाधीशों ने माना कि यद्यपि सी.पी.सी. भारत से अपील से संबंधित प्रक्रियाओं को विनियमित नहीं करता, फिर भी धारा 99 के अंतर्गत रेखांकित सिद्धांत ठोस है तथा न्याय को बढ़ावा देता है। इस प्रकार, यह माना गया कि माननीय न्यायाधीशों द्वारा ऐसी कार्यवाही की संभावना नहीं है, जिससे मामला अत्यधिक लम्बा खिंच जाए। आगे यह भी माना गया कि भले ही उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन पर आपत्ति को खारिज करने और दोनों कारणों पर सुनवाई की अनुमति देने में गलती हुई हो, फिर भी सुनवाई को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कथित संशोधन से न तो मामले की गुणवत्ता प्रभावित हुई, न ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव पड़ा है।
क्या 1914 में बनाई गई वसीयत वैध और वास्तविक थी
माननीय न्यायाधीशों ने कहा कि इस विशेष मुद्दे का निर्णय गिरि बाला के ससुर गणेश प्रसाद द्वारा 5 अप्रैल 1914 को निष्पादित की गई वसीयत के तथ्य और वास्तविकता पर निर्भर करता है, जो कि उनके दावे का आधार था। यह बताया गया कि मूल वसीयत खो गई थी और वसीयत की विषय-वस्तु को दो प्रमाणित प्रतियों द्वारा सत्यापित किया गया था, जिनकी प्रामाणिकता पर कोई विवाद नहीं था।
वसीयत के निष्पादन से संबंधित मामले के तथ्यों के संदर्भ में, जैसा कि इस लेख में पहले बताया गया है, यह पुष्टि की गई कि 1914 में बनाई गई प्रारंभिक वसीयत खो गई थी, इसलिए प्रतिवादी को वसीयत की विषय-वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इस साक्ष्य में दो प्रमाणित प्रतियां शामिल थीं – एक उस समय प्राप्त की गई जब मूल प्रति कलेक्टर के पास थी तथा दूसरी उच्च न्यायालय से प्राप्त की गई थी। यद्यपि इन प्रतियों की प्रामाणिकता और सटीकता पर कोई विवाद नहीं किया जा सका, तथापि वे केवल उस दस्तावेज की विषय-वस्तु की पुष्टि करते हैं, जिस पर 5 अप्रैल, 1914 को गणेश प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का आरोप है। तथापि, इस बात पर बल दिया गया कि ये प्रतियां यह साबित नहीं करतीं कि जिस मूल वसीयत के लिए ये प्रतियां बनाई गई थीं, उस पर वसीयतकर्ता ने हस्ताक्षर किए थे।
वसीयत के निष्पादन और वसीयत की प्रमाणित प्रतियों की प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए, माननीय न्यायाधीशों ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रकाश में इन पर विचार किया। उनके माननीय न्यायाधीशों ने वसीयत की वास्तविकता की घोषणा करते हुए, कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर अपना निर्णय दिया। सबसे पहले, प्रिवी काउंसिल ने मुंशी महावीर प्रसाद की गवाही पर भरोसा किया। उन्होंने अपने साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की कि उन्होंने वसीयत की एक अच्छी प्रतिलिपि बनाई थी और उसे गणेश प्रसाद को पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उनके हस्ताक्षर को दो गवाहों द्वारा सत्यापित (वेरीफाइड) किया गया। यद्यपि ये गवाह मर चुके थे, फिर भी जिस उप कलेक्टर को मूल वसीयत प्राप्त हुई थी, उसने इन गवाहों के बयान भी दर्ज किए थे और वह संतुष्ट था कि यह एक सच्ची प्रतिलिपि थी।
दूसरे, वसीयत की प्रमाणित प्रतियों से पता चला कि मूल दस्तावेज़ पर वसीयतकर्ता के दो हस्ताक्षर थे, जो 1911 की मूल वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षरों के समान थे। इसके अतिरिक्त, कई गवाहों को, जिन्होंने मूल दस्तावेज बरामद होने के तुरंत बाद देखा था, उस पर वसीयतकर्ता के दोनों हस्ताक्षरों को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह पाया गया कि कुछ गवाह 1911 की वसीयत के तहत न्यासी थे और उनकी गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का कोई कारण नहीं था। यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने 12 अक्टूबर, 1914 को उच्च न्यायालय में अपने आवेदन में उल्लेख किया था कि वे गणेश प्रसाद की लिखावट जानते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि 1914 की वसीयत पर हस्ताक्षर वास्तविक थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस दावे को खारिज कर दिया कि वसीयत की वैधता को स्वीकार करने में न्यासियों की कोई गुप्त मंशा थी और इसलिए, सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, उनके माननीय न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर सहमत हुए।
अंत में, बांदा के कलेक्टर श्री स्वान, जो गणेश प्रसाद की लिखावट से परिचित थे, ने भी 1914 की वसीयत पर उनके हस्ताक्षरों को पहचाना, जब डिप्टी कलेक्टर ने उसे उनके पास भेजा। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को दस्तावेज की बरामदगी और प्रामाणिकता के बारे में सूचित किया तथा उन्हें इसके प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की सलाह दी। इसलिए, साक्ष्य की समीक्षा करने के बाद, उनके माननीय न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न्यासियों के उद्देश्यों या प्रस्तुत किए गए प्रमाण को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं था और इस प्रकार, उन्होंने वसीयत की प्रामाणिकता को स्वीकार कर लिया।
क्या गिरि बाला का विवादित गांव पर वैध अधिकार था
वसीयत की वास्तविकता का निर्धारण करने के बाद, माननीय न्यायाधीशों ने वसीयत की विषय-वस्तु का विश्लेषण करना शुरू किया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्या गिरि बाला का विवादित गांव पर वैध अधिकार था। यह पाया गया कि गणेश प्रसाद और उनके बेटे के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और यह स्पष्ट और निर्विवाद था। इसी दुश्मनी के कारण गणेश प्रसाद ने 1911 में वसीयत बनाकर अपने बेटे और उसके परिवार को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। हालाँकि, जब गणेश प्रसाद बीमार पड़े, तो उन्होंने संभवतः इस रुख पर पुनर्विचार किया और अपने रिश्तेदारों और आश्रितों के लिए प्रावधान करने हेतु 1914 में एक नई वसीयत बनाई।
1914 में बनाई गई वसीयत की विषय-वस्तु के अनुसार, वसीयतकर्ता ने संपत्ति की आय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र को आजीवन अधिकार प्रदान किया, तथा उसे संपत्ति का निपटान करने का अधिकार नहीं दिया। वसीयत में आगे यह भी प्रावधान किया गया था कि उसके बेटे की मृत्यु पर संपत्ति उसके बेटे के बच्चे को मिलेगी और बच्चे के न होने पर यह उसकी पत्नी को मिलेगी। 1914 की वसीयत में गणेश प्रसाद की मालकिन जयराज कुँअर के भरण-पोषण का भी प्रावधान किया गया था।
उनके माननीय न्यायाधीशों ने पाया कि वसीयत की विषय-वस्तु उचित थी और उन्होंने कहा कि जब 1914 में मृतक के घर से वसीयत बरामद की गई थी, तो किसी ने भी यह नहीं कहा था कि यह जाली है। इसके अलावा, जिन लोगों ने यह दावा किया था कि इस मामले के लंबित रहने के दौरान 1914 की वसीयत जाली थी, उन्होंने इस दावे के प्रमाण के रूप में कोई साक्ष्य नहीं दिया था, और इसलिए, उनके माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय से सहमत थे, कि वसीयत की वैधता गिरि बाला के पक्ष में बरकरार रखी जानी चाहिए, क्योंकि विवादित गांव पर उनका वैध अधिकार था।

क्या वसीयत के तहत दी गई संपत्ति पैतृक है और क्या गणेश प्रसाद के बेटे का उसमें उनके साथ संयुक्त हित था
प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने उल्लेख किया कि गणेश प्रसाद को यह संपत्ति उनके नाना जदु राम से उपहार के रूप में विरासत में मिली थी। इसलिए, प्रिवी काउंसिल के सामने यह प्रश्न आया कि क्या इस संपत्ति को पैतृक माना जाएगा, जिससे उसके बेटे को जन्म से ही इसमें हिस्सेदारी मिल जाएगी। यह उल्लेख किया गया कि इस मुद्दे पर भारतीय न्यायपालिका की अलग-अलग राय मौजूद है और उन्होंने अपनी टिप्पणियों के समर्थन में करुप्पाई नचियार बनाम शंकरनारायणन केट्टी (1903), हम प्रताप एवं अन्य बनाम जमना प्रसाद एवं अन्य (1907), तथा विश्वमथ प्रसाद साहू बनाम गंजधर प्रसाद (1917) जैसे मामलों का हवाला दिया। इस मामले की व्यावहारिक प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए, माननीय न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रश्न अनिश्चित नहीं रहना चाहिए।
यह ध्यान दिया गया कि अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के अनुसार, एक बेटी के बेटे को उसके नाना से विरासत में मिली संपत्ति, पैतृक संपत्ति है। उन्होंने अपना तर्क “पैतृक संपत्ति” शब्द के आधार पर तैयार किया, जैसा कि राजा चेलिकानी वेंकैयाम्मा गारू बनाम राजा चेलिकानी वेंकटरामनय्याम्मा (1902) के फैसले में परिभाषित किया गया था। इस मामले में, पोते, जो एक बेटी के बेटे थे, ने अपने नाना से संपत्ति ले ली और उत्तरजीविता के अधिकार के साथ उस पर संयुक्त रूप से अधिकार जमा लिया। उनके माननीय न्यायाधीशों ने पाया कि इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा यह था कि संपत्ति उत्तरजीविता के अधिकार के साथ पारित की गई थी या इसके बिना। यह निर्णय लिया गया कि संपत्ति उत्तरजीविता के नियम द्वारा शासित थी और विधवा के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें एक ही समय में और एक ही शीर्षक से संपत्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने इसे अन्य संयुक्त संपत्ति के समान ही धारण किया। उनके माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि इस विशेष मामले में, “पैतृक संपत्ति” शब्द को दिया गया अर्थ प्राकृतिक था, जो पूर्वजों से विरासत में मिली संपत्ति को दर्शाता है, न कि तकनीकी अर्थ, जैसा कि हिंदू कानूनों के तहत प्रदान किया गया है, जहां एक पुत्र को अपने पिता के साथ जन्म से ही उसमें हिस्सेदारी प्राप्त होती है। इस विशेष मामले पर न तो कभी बहस की गई और न ही प्रिवी काउंसिल द्वारा इस पर निर्णय लिया गया।
यह भी देखा गया कि बाद में अतर सिंह बनाम ठाकर सिंह (1908) मामले में दिया गया निर्णय, इस विशेष मुद्दे के लिए प्रासंगिक था। इस मामले में, यह माना गया कि जब तक संपत्ति “पुरुष वंश में एक प्रत्यक्ष पुरुष पूर्वज से वंश द्वारा” विरासत में नहीं मिलती है, तब तक संपत्ति को हिंदू कानून के तहत पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, यह मामला उस संपत्ति के संदर्भ में था जो पुरुष संपार्श्विक (कॉलेटरल) से प्राप्त हुई थी और नाना से विरासत में नहीं मिली थी और पंजाब के रीति-रिवाजों के अनुरूप भी थी। यह भी बताया गया कि यह तर्क नहीं दिया गया कि पंजाब की प्रथा, उस मामले में उनके समक्ष प्रस्तुत मामले के संबंध में हिंदू कानून से भिन्न थी।
हिंदू कानून के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, पैतृक संपत्ति का अर्थ वह संपत्ति है जो किसी व्यक्ति को उसके पिता, या पिता के पिता, या पिता के पिता के पिता से विरासत में मिलती है। यह संपत्ति स्वतः ही उत्तराधिकार के रूप में उसके पुरुष वंशजों को प्राप्त हो जाती है, और वे इसे सहदायिक संपत्ति के रूप में, उत्तरजीविता के अधिकार के साथ ग्रहण करते हैं। हालाँकि, वर्तमान मामले में अपील के तहत प्रश्न यह है कि क्या बेटे को पिता के नाना से पिता को विरासत में मिली संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है।
मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने जन्म से प्राप्त अधिकारों को पैतृक या दादा-दादी की संपत्ति तक सीमित कर दिया है। कोलब्रुक ने मिताक्षरा ग्रन्थ का अनुवाद किया और उन्होंने “पैतृक संपत्ति” को मातृ संपत्ति के संदर्भ में नहीं बल्कि दादा-दादी की संपत्ति के संदर्भ में परिभाषित किया। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि विज्ञानेश्वर द्वारा प्रयुक्त शब्द “पितामह”, जो कि मूल संस्कृत शब्द है, का अर्थ विशेष रूप से “पिता का पिता” है और इसमें मातृ पुरुष पूर्वज शामिल नहीं हैं। मिताक्षरा के आगे के अध्यायों में कहा गया है कि यह पैतृक दादा की संपत्ति है, जिसमें पुत्र को पिता के साथ जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है। जब कोलब्रुक ने “पैतृक संपदा” शब्द का प्रयोग किया, तो वास्तव में वह दादा-दादी की संपदा की ओर संकेत कर रहे थे। इसलिए, हिंदू कानून के तहत पैतृक संपत्ति, जिसमें पुत्र को जन्म से ही संपत्ति प्राप्त हो जाती है, केवल उस संपत्ति को संदर्भित करती है जो पुरुष वंश के माध्यम से पुरुष पूर्वजों से प्राप्त होती है।
सामान्य अर्थ में “पूर्वज” शब्द में माता और पिता दोनों पक्षों के पूर्वज शामिल थे। हालाँकि, हिंदू कानून के तहत, “पैतृक” संपत्ति, जिसमें पुत्र को अपने पिता के साथ जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है, केवल उन संपत्तियों को संदर्भित करती है जो पिता या पैतृक वंश में अन्य पुरुष संबंधियों से विरासत में मिलती हैं, जैसा कि मूल मिताक्षरा पाठ के तहत प्रावधान किया गया है। इसलिए उनके माननीय सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि सामान्य या शाब्दिक अर्थ में “पैतृक” शब्द का प्रयोग करने से भ्रम उत्पन्न हुआ था।
इसलिए, “पैतृक संपत्ति” शब्द की उपर्युक्त व्याख्या के संबंध में, उनके माननीय न्यायालय ने माना कि चूंकि गणेश प्रसाद को विरासत में जो संपत्ति मिली थी, वह उनके नाना से थी, इसलिए ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि गणेश प्रसाद को संपत्ति का निपटान करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्रवधू गिरि बाला के पक्ष में जो वसीयत तैयार की है, उस पर उनका बेटा या कोई अन्य व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता। जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उनकी अंतिम वसीयत की शर्तें लागू हो गईं और कालिंजर तिरहटी गांव और संपूर्ण संपत्ति के सभी मालिकाना अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए। उस गांव की बिक्री से, उसके पति के खिलाफ निष्पादन की कार्यवाही में, उसके हक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
निर्णय के बाद की स्थिति
प्रिवी काउंसिल द्वारा इस मामले में अपना निर्णय सुनाए जाने के बाद, एक मिसाल कायम हुई जिसका अनुसरण विभिन्न अदालतों में बाद में आए अनेक मामलों में किया गया।
डॉ. मुहम्मद सुहैल बनाम चांसलर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य (1994) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चयन समिति के गठन की वैधता और क्या इसके गठन में अनियमितता का उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 66 के तहत ऐसी समिति द्वारा किए गए चयन पर कोई प्रभाव पड़ा था, के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मुहम्मद हुसैन खान बनाम बाबू किश्व नंदन सहाय (1937) के इस मामले का संदर्भ दिया था। अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 66 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रावधान समान विषय-वस्तु पर आधारित हैं। इसी संदर्भ में न्यायालय ने मुहम्मद हुसैन खान बनाम बाबू किश्व नंदन सहाय (1937) के मामले का उल्लेख किया और कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 का उद्देश्य यह है कि मात्र दोष या अनियमितताएं अपील में डिक्री को उलटने या बदलने का आधार नहीं होंगी। दूसरे शब्दों में, यह धारा मात्र दोष या अनियमितता को स्वीकार करती है, लेकिन भौतिक अवैधता को ख़राब नहीं करती है।
सीआईटी बनाम राम रक्षपाल, अशोक कुमार (1968) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को प्राप्त संपत्ति के उपयोग से उत्पन्न आय को हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) की आय के हिस्से के रूप में या पुत्र की अलग संपत्ति के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने मुहम्मद हुसैन खान बनाम बाबू किश्व नंदन सहाय (1937) के मामले का उल्लेख करते हुए हिंदू कानून के इस सुस्थापित नियम की पुनः पुष्टि की कि किसी व्यक्ति को पैतृक वंश में तीन प्रत्यक्ष पूर्वजों अर्थात् पिता, दादा या परदादा में से किसी से विरासत में मिली संपत्ति उसके पुरुष वंशजों के लिए पैतृक संपत्ति कहलाती है। उनके बेटे को जन्म से ही इस संपत्ति में साझा हिस्सेदारी प्राप्त थी। यह संपत्ति भी उसके पुरुष उत्तराधिकारियों के साथ सहदायिकता में रखी जाती है तथा इस संपत्ति पर उत्तरजीविता का नियम लागू होता है।

निष्कर्ष
मुहम्मद हुसैन खान बनाम बाबू किश्व नंदन सहाय (1937) का मामला प्रासंगिक है, क्योंकि इसने हिंदुओं पर लागू कानूनों के तहत पैतृक संपत्ति की परिभाषा से संबंधित भ्रम को हल कर दिया। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने, इस विशेष मुद्दे पर निर्णायक (कंक्लूसिवली) निर्णय लेने के उद्देश्य से, मिताक्षरा विधि विद्यालय से संबंधित अनुवादित पाठ का विश्लेषण किया। पाठ के गहन विश्लेषण के बाद प्रिवी काउंसिल ने इस भ्रम को दूर कर दिया और कहा कि पैतृक संपत्ति में केवल वही संपत्तियां शामिल हैं जो परिवार के पितृ पक्ष के पुरुष संबंधियों से विरासत में मिली हों। परिणामस्वरूप, भौतिक पक्ष के पुरुष संबंधियों से विरासत में प्राप्त कोई भी संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं थी और इसलिए, उसे उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में निपटाया जा सकता था, जिसे वह दी गई थी। यह हिंदू उत्तराधिकार और विरासत कानून के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 99 क्या है?
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 के अनुसार, मामले की कार्यवाही में किसी त्रुटि, दोष या अनियमितता के आधार पर किसी डिक्री को उलटा, परिवर्तित या प्रतिप्रेषित (रिमांडेड) नहीं किया जाना चाहिए, यदि ऐसी त्रुटि, दोष या अनियमितता मामले के गुण-दोष या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रक्रियात्मक या औपचारिक मुद्दा अन्यथा कानूनी और उचित निर्णयों पर हावी न हो। हालाँकि, इस धारा के प्रावधान के अनुसार, यदि मामले में आवश्यक पक्ष शामिल नहीं है तो धारा 99(1) का प्रावधान लागू नहीं होता है। आवश्यक पक्ष वह व्यक्ति होता है जिसे मामले में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि विवाद को सुलझाने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए, यदि मामले में कोई आवश्यक पक्ष शामिल नहीं है, तो उसी के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 99 का प्रावधान यह पुष्टि करता है कि प्रक्रियाओं में छोटी-मोटी गलतियों से न्यायिक निर्णय की अखंडता प्रभावित नहीं होती, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि मामले में सभी महत्वपूर्ण पक्ष भाग लें।
वसीयत क्या है और भारत में वसीयत का निष्पादन किस कानून के तहत होता है?
वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा यह निर्धारित करने के लिए लिखा और हस्ताक्षरित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति और अन्य परिसंपत्तियों का निपटान कैसे किया जाना चाहिए। भारत में वसीयत कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन्हें किसी भी प्रारूप में तैयार किया जा सकता है। इन्हें स्टाम्प पेपर पर तैयार करना आवश्यक नहीं है तथा इन्हें टाइप किया जा सकता है या हस्तलिखित भी किया जा सकता है। हालाँकि, हस्तलिखित वसीयत को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इसे अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना कम होती है। भारत में वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होती है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, वसीयत किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती है जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो और नाबालिग न हो।
उत्तराधिकार का क्या अर्थ है और भारत में कौन सा कानून हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है?
उत्तराधिकार को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसके तहत भूमि, संपत्ति और घर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं, ताकि ऐसी परिसंपत्तियों पर परिवार का स्वामित्व बना रहे। हिंदू उत्तराधिकार कानून में उन प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है जिनके द्वारा हिंदू परिवारों के बीच परिसंपत्तियों का हस्तांतरण किया जाता है। भारत में यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा शासित है। इस अधिनियम की धारा 2 अधिनियम की प्रयोज्यता को रेखांकित करती है। इसमें प्रावधान किया गया है कि यह अधिनियम हिंदू धर्म या इसके विभिन्न रूपों (वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज सहित), बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, जब तक कि ऐसा व्यक्ति यह साबित नहीं कर देता कि वह हिंदू कानून या रीति-रिवाज से बंधा नहीं है।
पैतृक संपत्ति क्या है और यह स्व-अर्जित संपत्ति से किस प्रकार भिन्न है?
सामान्य अर्थ में “पूर्वज” शब्द में माता और पिता दोनों पक्षों के पूर्वज शामिल होते हैं। हालांकि, हिंदू कानून के तहत, पैतृक संपत्ति के संबंध में, जहां पुत्र को जन्म से ही अपने पिता के साथ हिस्सेदारी मिलती है, केवल ऐसी संपत्तियों पर ही विचार किया जाता है जो पिता या पैतृक वंश में अन्य पुरुष संबंधियों से विरासत में मिली हों। दूसरी ओर, स्व-अर्जित संपत्ति वह है जिसे किसी व्यक्ति ने अपने साधनों से खरीदा हो। ऐसी स्थिति हो सकती है कि स्व-अर्जित संपत्ति पैतृक संपत्ति बन जाए या इसके विपरीत भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा स्व-अर्जित हो जाता है, यदि उसे संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित और वितरित कर दिया जाए। दूसरी ओर, स्व-अर्जित संपत्ति पैतृक संपत्ति में बदल जाती है, जब आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई विभाजन नहीं होता है।
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) क्या है?
हिंदू कानून के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एक अलग कानूनी व्यक्तित्व है। इसमें एक ही पूर्वज के प्रत्येक प्रत्यक्ष वंशज और उनकी पत्नियाँ शामिल हैं। एचयूएफ एक कानूनी इकाई के रूप में कार्य करता है, जिसमें संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व और आय का एक सामान्य स्रोत होता है।
सहदायिक का क्या अर्थ है और हिंदू कानून के अनुसार सहदायिक कौन है?
संपत्ति को नियंत्रित करने वाले भारतीय कानून के तहत, सहदायिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका जन्म के समय से ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। इससे पहले, ऐसे अधिकार केवल हिंदू अविभाजित परिवार के पुरुष सदस्यों को ही दिए जाते थे। हालाँकि, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों को सहदायिक के समान संपत्ति अधिकार दिए गए। अब, पुरुष के साथ-साथ महिला एचयूएफ सदस्य भी सहदायिक हो सकते हैं।
हिंदू कानून के तहत सहदायिक की स्थिति कैसे बदल गई?
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) में सहदायिकों के अधिकारों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। इससे पहले नियम यह था कि केवल बेटों को ही सहदायिक का अधिकार होगा तथा बेटियों को जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। इस संशोधन ने बेटियों के पक्ष में, उन्हें सहदायिक के समान अधिकार प्रदान करके, इस ऐतिहासिक लैंगिक पक्षपात (बायस) का प्रभावी ढंग से जवाब दिया है और उसका निवारण किया है। इस संशोधन के तहत बेटियों को, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, पैतृक संपत्ति पर बेटों के समान कानूनी अधिकार दिए गए। उन्हें जन्म से सहदायिक के रूप में मान्यता दी जाती है, जिससे उन्हें परिवार की पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन एचयूएफ के भीतर अधिक समावेशी और न्यायसंगत कानूनी ढांचे को सुनिश्चित करता है, जो लैंगिक न्याय और समानता के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप है। किसी भी एचयूएफ के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, सहदायिकों या उनकी कानूनी स्थिति और अधिकारों से संबंधित अवधारणा की पर्याप्त समझ होना आवश्यक हो जाता है। सहदायिक में संपत्ति के विभाजन के दौरान, कानूनी प्रणालियाँ सहदायिकों के बीच हिस्से को वितरित करने के तरीके के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो इसका हकदार है, उसे समान हिस्सा मिले। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों को लैंगिक समानता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा सकता है। पुत्रियों को पुत्रों के समान संपत्ति अधिकार प्रदान करके, यह संशोधन सहदायिकता प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनिधित्व के प्रति अधिक निष्पक्ष और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। यह प्रगतिशील कानूनी परिवर्तन न केवल महिलाओं को सशक्त बनाता है, बल्कि पैतृक संपत्ति के वितरण में न्याय सुनिश्चित करके संयुक्त परिवार प्रणाली को भी मजबूत बनाता है।
संदर्भ







