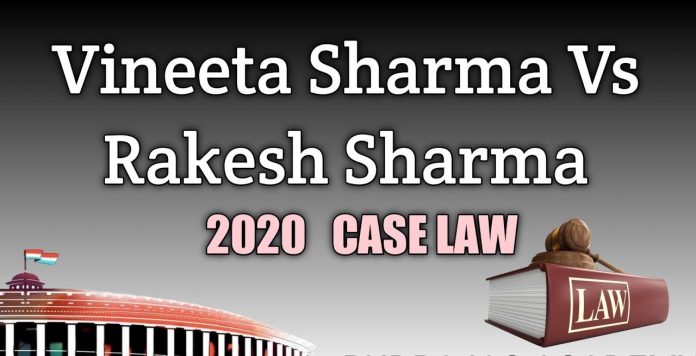यह लेख Arya Senapati द्वारा लिखा गया है । यह लेख विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के हालिया ऐतिहासिक मामले का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जिसने अंततः हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में जोड़ी गई धारा 6 के पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव के प्रश्न को सुलझा दिया। विश्लेषण में तथ्यात्मक मैट्रिक्स, कानूनी मुद्दे, उन्नत (एडवांस्ड) तर्क, निर्णय, अन्य संबंधित मामले और मामले में शामिल कानूनी सिद्धांत भी शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
सकारात्मक कार्रवाई भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग में निहित प्राथमिक संवैधानिक सिद्धांतों में से एक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है और अनुच्छेद 15 विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है। लिंग के संदर्भ में, संविधान लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति की गारंटी देता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, संविधान विशेष कानूनों और नीतियों के निर्माण की आवश्यकता बताता है जो महिलाओं पर वर्षों से चल रहे प्रणालीगत (सिस्टेमिक) उत्पीड़न और असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कार्य करेंगे।
संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में, हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति, जिसे अक्सर सहदायिक (कॉपरसनरी) संपत्ति कहा जाता है, कानून की मिताक्षरा प्रणाली द्वारा शासित होती है। यह प्रणाली अपने दृष्टिकोण में रूढ़िवादी है और महिलाओं को सहदायिक का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देती है और इस प्रकार संपत्ति में उनके हित को सीमित करती है। यह विचार प्रारंभिक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में परिलक्षित हुआ था, जो बिना वसीयत के उत्तराधिकार (किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति का उत्तराधिकार जो बिना किसी वसीयतनामा के मर जाता है) से निपटता है और केवल पुरुष सहदायिकों के हितों को शामिल करता है।
इस लैंगिक अन्याय को ठीक करने के लिए, संसद ने हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 लाया, जिसने मूल अधिनियम की धारा 6 को प्रतिस्थापित किया। नए संशोधित प्रावधान ने महिलाओं को सहदायिक अधिकार और हित प्रदान किए और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने पुरुष समकक्षों के समान संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हों। इसमें कहा गया है कि बेटों की तरह ही बेटियों को भी जन्म से सहदायिक अधिकार प्राप्त होंगे और संपत्ति के प्रति बेटियों को भी बेटों के समान ही अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। प्रावधान की प्रयोज्यता (एप्लीकेशन) के संदर्भ में प्रावधान ने कई अन्य पहलुओं पर भी विचार किया।
संशोधन के लागू होने के साथ ही न्यायालयों ने इसका एक प्रगतिशील कदम के रूप में स्वागत किया है, लेकिन इसने न्यायिक व्याख्या के क्षेत्र में बहुत भ्रम भी पैदा किया है। न्यायालयों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह प्रावधान पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा या भावी (प्रॉस्पेक्टिव) रूप से। एक सामान्य नियम के रूप में, सभी संशोधनों का भावी प्रभाव होता है जब तक कि प्रावधान में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पूर्वव्यापी प्रयोज्यता की संभावना का उल्लेख न किया गया हो। व्याख्या को लेकर इस भ्रम के कारण विभिन्न न्यायालयों और पीठों द्वारा अलग-अलग विचार सामने आए। जबकि कुछ का मानना था कि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, पर बहुमत ने इस विचार को नकार दिया।

इसने प्रकाश बनाम फुलवती (2015) और दानम्मा बनाम अमर (2018) जैसे मामलों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जो अन्य प्रश्नों से भी निपटते हैं जैसे ‘क्या प्रावधानों की प्रयोज्यता के लिए संशोधन के प्रारंभ के दौरान पिता और पुत्री दोनों का जीवित रहना आवश्यक है?’ और ‘क्या संशोधन शुरू होने के बाद अदालतों में लंबित मामलों पर प्रावधान लागू हो सकते हैं?’। जबकि निर्णय एक-दूसरे के साथ टकराव में थे, सवालों पर अंतिम फैसला या अंतिम व्याख्या विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के मामले में आई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रावधान प्रकृति में भावी नहीं है; बल्कि यह प्रकृति में पूर्वव्यापी है और इसे उसी के अनुसार समझा या लागू किया जाना चाहिए। इसने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के लागू होने के लिए पिता और पुत्री दोनों का कानून के प्रारंभ के दौरान जीवित होना आवश्यक नहीं है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- धर्म का हिंदू विचार वैदिक आर्यों के सिद्धांतों से प्रभावित है। हिंदू कानूनों के संदर्भ में, दो प्राथमिक विचारधाराएं हैं, जो मिताक्षरा और दयाभाग हैं। मिताक्षरा को बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्रविड़ में विभाजित किया गया है। इसलिए मिताक्षरा विचारधारा क्षेत्रवार (रीजन वाइस) लागू होता है।
- जब हिंदू कानून के कुछ पहलुओं पर राज्य चुप रहते हैं, तो न्यायिक निर्णय उन अंतरालों को भर देते हैं और इसलिए हिंदू कानून कभी स्थिर नहीं रहा, बल्कि प्रगतिशील रहा है। समय बीतने के साथ, संहिताकरण (कोडिफिकेशन) की आवश्यकता महसूस की गई, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के लिए, ताकि कुछ विसंगतियों और बेईमान सिद्धांतों को मिटाया जा सके।
- संवैधानिक रूप से महिलाओं को समान दर्जा दिया गया है और लिखित कानून संवैधानिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय-समय पर संशोधनों के अधीन था। सबसे हालिया संशोधन 2005 का संशोधन था, जिसने सहदायिक संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में बेटियों और बेटों को समान अधिकार दिए।
मामले के तथ्य
इस मामले में मृतक सहदायिक श्री देवदत्त शर्मा हैं, और उनकी मृत्यु के बाद उनके पीछे एक विधवा, एक बेटी और तीन बेटे रह गए। उनका निधन 11 दिसंबर, 1999 को हुआ। उनका एक बेटा, जो अविवाहित था, 1 जुलाई, 2001 को उसकी मृत्यु हो गई थी । इसके बाद, बेटी विनीता शर्मा, जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, ने सहदायिक संपत्ति में 1/4 हिस्सा पाने का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया।
उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने उसके दावे को अस्वीकार कर दिया और कहा कि, यह देखते हुए कि उसके पिता का निधन 1999 में हुआ था, जो कि संशोधन लागू होने से बहुत पहले की बात है, उसे सहदायिक नहीं माना जा सकता और इसलिए परिवार की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, यह देखते हुए कि वह विवाहित थी, उसका परिवार की संपत्ति पर कोई दावा नहीं रह गया है क्योंकि वह अब संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं है। विनीता शर्मा ने अपने भाइयों राकेश शर्मा और सत्येंद्र शर्मा के साथ-साथ उनकी माँ पर भी मुकदमा दायर किया। उसने परिवार में अपने जन्म के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति पर सहदायिक अधिकार का दावा किया। कानून सहदायिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जन्म को वैध स्रोत मानता है और इसकी गारंटी देता है।
वादी विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय से व्यथित थी, जिसमें उसे सहदायिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया था। उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से निर्णय को चुनौती दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने माना कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 6 वर्तमान स्थिति पर लागू नहीं होगी क्योंकि संशोधन के लागू होने के दौरान विनीता शर्मा के पिता जीवित नहीं थे। यह निर्णय प्रकाश बनाम फुलवती (2015) के फैसले पर आधारित था, जिसमें यह माना गया था कि संशोधित प्रावधानों को लागू करने के लिए संशोधन 2005 के प्रारंभ के दौरान पिता और बेटी दोनों को जीवित रहना चाहिए। इस निर्णय ने बेटी को व्यथित कर दिया, जिसके कारण उसने मामले पर पुनर्विचार करने और निर्णय पर पहुंचने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।
मामलों की सूची और निर्णय
इस मामले के फैसले को समझने के लिए, इस कानूनी मुद्दे की पिछली न्यायिक यात्रा को समझना महत्वपूर्ण है, जो 2005 के संशोधन द्वारा संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों के पूर्वव्यापी प्रोज्याता के बारे में है। मोटे तौर पर दो मामले हैं जिनमें न्यायालय ने इस मामले पर अपनी राय को पुष्ट किया और जो इस मुद्दे का सार है। जिन दो मामलों की जांच की जानी चाहिए, वे निम्नलिखित हैं:
प्रकाश बनाम फुलवती (2015)
प्रकाश बनाम फूलवती (2015) के मामले में, फूलवती, जो मृतक की बेटी थी, ने अपने पिता की सहदायिक की बेटी होने के आधार पर संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगा था। विभाजन और अलग कब्जे के लिए एक मुकदमे में, उसने अपने मृत पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में 1/7वां हिस्सा मांगा। मुकदमे के दौरान, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 पारित हुआ, जिसने बेटों और बेटियों को समान सहदायिक अधिकार दिए और कहा कि बेटियों को जन्म से परिवार की सहदायिक माना जाएगा। संशोधन के बाद, फूलवती ने सहदायिक संपत्ति में बराबर हिस्से का दावा किया।
विचारण न्यायालय ने फूलवती को बराबर हिस्से देने से इनकार कर दिया। इस फैसले को उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उसकी चुनौती इस आधार पर थी कि नए संशोधन के अनुसार, वह भी अपने भाइयों की तरह समान सहदायिक है और सहदायिक संपत्ति के संबंध में उसके अपने भाइयों के समान अधिकार और जिम्मेदारियां हैं। इस सिद्धांत के आधार पर, उसे अपने भाइयों के बराबर हिस्सा मिलने की मांग करी। बचाव पक्ष, यानी उसके भाई, ने तर्क दिया कि संशोधित प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि वादी के पिता की मृत्यु संशोधन के लागू होने से पहले हो गई थी, और इसलिए पुराने प्रावधानों के आधार पर ही हिस्सों का निर्धारण किया जाना चाहिए। बचाव पक्ष के अनुसार, उत्तराधिकार के खुलने की तिथि पर लागू प्रावधान ही वादी के हिस्सों का निर्धारण करेगा।

उच्च न्यायालय ने वादी फूलवती के पक्ष में फैसला दिया और यह माना कि जब कोई मुकदमा संशोधन के लागू होने के समय लंबित हो, तो संशोधित प्रावधान अंतिम निर्णय लेने के लिए लागू होंगे, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जी. शेखर बनाम गीता और अन्य (2009) के मामले में कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में कहा कि किसी कानून में हुए बदलाव उन मुकदमों पर भी लागू होंगे जो लंबित हैं, और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं माना जाएगा। इसलिए, संशोधित प्रावधानों के आधार पर, इस मामले में वादी, जो कि बेटी है, संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार है और जन्म से ही सहदायिक है। इसमें यह भी कहा गया कि पिता का अधिनियम के लागू होने के समय जीवित होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है। इसका एकमात्र अपवाद वह विभाजन है जो 20.12.2004 से पहले प्रभावी हो चुका हो और जो पंजीकृत विभाजन विलेख (डीड) या न्यायालय के अंतिम निर्णय द्वारा सुनिश्चित हो चुका हो। लेकिन वर्तमान मामला इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता।
इस फैसले से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा प्रावधान के पूर्वव्यापी उपयोग को चुनौती दी और यह तर्क दिया कि चूंकि वादी के पिता संशोधन के लागू होने के समय जीवित नहीं थे, इसलिए उसे सहदायिक का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। प्रतिवादी, फूलवती, ने तर्क दिया कि यह कानून एक सामाजिक कानून है जो महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में बराबरी दिलाने के लिए बनाया गया है, इसलिए न्याय की दृष्टि से इस प्रावधान के पूर्वव्यापी उपयोग पर जोर देना आवश्यक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को केवल प्रावधान के प्रतिगामी उपयोग के मुद्दे तक सीमित रखा और कहा कि 2005 का संशोधन इस मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी का पिता संशोधन के लागू होने के समय जीवित नहीं था। सहदायिक के अधिकार पाने के लिए पिता का जीवित होना आवश्यक है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि जब संशोधन लागू हुआ, तब वह सहदायिक की बेटी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता का संशोधन से पहले ही निधन हो चुका था और उसे सहदायिक नहीं माना जा सकता।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को कायम रखा कि आम तौर पर कोई संशोधन पूर्वव्यापी रूप से तब तक लागू नहीं होता जब तक कि प्रावधान में स्पष्ट या निहित रूप से इसके विपरीत कुछ न कहा गया हो। प्रावधानों के इस प्रकार की प्रयोज्यता की व्याख्या करते समय न्यायालय को प्रावधानों की भाषा को सीधे पढ़ने तक सीमित रहना चाहिए और प्रावधानों के उद्देश्य और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इसकी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के प्रावधानों की भाषा और पाठ में पूर्वव्यापी प्रयोज्यता की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि सहदायिक के अधिकार बेटी को संशोधन के लागू होने की तिथि से मिलते हैं। अधिनियम के प्रावधानों की सरल भाषा में कहीं भी इसके विपरीत कुछ नहीं कहा गया है।
सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि भले ही यह कानून महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया हो, लेकिन सामान्य नियम के तहत इसे केवल भविष्य के लिए लागू किया जा सकता है। सामाजिक कानूनों का भी पूर्वव्यापी प्रयोज्यता नहीं होती जब तक कि प्रावधान में इसे स्पष्ट या निहित रूप से नहीं कहा गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, प्रावधान की व्याख्या उस संदर्भ और भाषा के आधार पर की जानी चाहिए और यदि कोई अस्पष्टता होती है, तो न्यायालय को प्रावधान को तर्कसंगत अर्थ देना चाहिए। जब प्रावधान और व्याख्या के बीच कोई टकराव होता है, तो प्रावधान की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में सही अर्थ कानून बनाने वाले के उद्देश्य और मंशा से निकाला जाना चाहिए।
इन कारणों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संशोधन के तहत अधिकार केवल उन बेटियों को मिलेंगे जिनके पिता संशोधन के लागू होने की तिथि यानी 9 सितंबर, 2005 को जीवित थे। बेटी के जन्म की तिथि महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पिता का जीवित होना ही महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए, प्रतिवादी फूलवती सहदायिक नहीं थी और उसे समान हिस्सेदारी का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया।
दानम्मा उर्फ सुमन सुरपुर एवं अन्य बनाम अमर एवं अन्य (2018)
इस मामले में, मृतक, श्री गुरलिंगप्पा सावदी, अपने पीछे एक विधवा और चार बच्चे छोड़ गए, जिनमें से उनके दो बेटे और दो बेटियाँ थीं। अपीलकर्ता, दानम्मा, मृतक की बेटियों में से एक थी। वर्ष 2002 में, मृतक के बेटों में से एक के बेटे अमर ने विभाजन और संपत्ति के अलग कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। उन्होंने दोनों बेटियों के संपत्ति पर समान अधिकार के दावों को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दोनों बेटियों का जन्म हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अधिनियमन से पहले हुआ था, और इसलिए, वे सहदायिक की स्थिति या संपत्ति में किसी भी हित का दावा नहीं कर सकती हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, यह देखते हुए कि उन्होंने अपनी शादी के दौरान दहेज प्राप्त किया था, उनका हिस्सा प्रभावी रूप से पूरा हो गया था।
विचारण न्यायालय ने दहेज से संबंधित तर्क को खारिज कर दिया लेकिन इस तथ्य को स्वीकार किया कि बेटियों को सहदायिक नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उनका जन्म हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले हुआ था। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। विचारण न्यायालय ने वर्ष 2007 में अपना फैसला सुनाया लेकिन मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, 2005 का संशोधन पारित किया गया, जिसने बेटियों के सहदायिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया लेकिन न तो विचारण न्यायालय और न ही उच्च न्यायालय ने संशोधन पर कोई ध्यान दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर दानम्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या बेटियों को इस आधार पर सहदायिक संपत्ति के उनके हिस्से से वंचित किया जा सकता है कि वे अधिनियम के लागू होने से पहले पैदा हुई थीं। इसमें कहा गया है कि किसी प्रावधान की भाषा की व्याख्या पाठ और संदर्भ को सरलता से पढ़कर की जानी चाहिए। इस नियम को लागू करने से यह स्पष्ट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) भावी प्रकृति की है, लेकिन अन्य सभी उपधाराओं का प्रभाव पूर्वव्यापी होगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि विधानमंडल की मंशा के आधार पर प्रावधानों की व्याख्या को सामंजस्यपूर्ण ढंग से बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस मामले में विधानमंडल की मंशा हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान पहुंच प्रदान करना है। इस तर्क के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बेटियों को संपत्ति में उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे संशोधन के लागू होने के दौरान और उसके बाद जीवित थीं। इसलिए, न्यायालय ने माना कि संशोधन के लागू होने के दौरान बेटी का जीवित होना सहदायिक संपत्ति में उनके हिस्से का पता लगाने के लिए पर्याप्त है। न्यायालय ने जिस अगले मुद्दे पर विचार किया वह यह था कि क्या बेटियों को सहदायिक संपत्ति में समान पहुंच है और क्या वे बेटों की तरह जन्म से ही सहदायिक हो जाती हैं। प्रावधानों की भाषा की शाब्दिक व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि बेटियां बेटों की तरह ही सहदायिक हो जाती हैं और इसलिए उन्हें बेटों के समान ही हिस्सेदारी मिलती है। यह देखते हुए कि कानून के पीछे की मंशा महिलाओं को सहदायिक होने का समान आधार प्रदान करना है, यह माना जाना चाहिए कि उन्हें बेटों की तरह ही जन्म से ही सहदायिक होना चाहिए।
इस निर्णय ने बड़ी उलझन पैदा कर दी क्योंकि निर्णय ने फुलवती मामले के अनुपात को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि एक बेटी को हिंदू संयुक्त परिवार में सहदायिक होने के लिए, संशोधन के प्रारंभ के दौरान पिता और बेटी दोनों को जीवित रहना चाहिए, जिससे यह सिद्धांत मजबूत हो गया कि संशोधन केवल जीवित सहदायिकों की जीवित बेटियों पर लागू है। अस्पष्टता यह है कि दानम्मा के मामले में, अपीलकर्ता के पिता की मृत्यु 2001 में हो गई थी, जो संशोधन से पहले की बात है लेकिन उसके बाद भी, सर्वोच्च न्यायालय ने बेटी को बराबर हिस्सेदारी दी। एक विशेष सिद्धांत को कायम रखने और न्यायालय द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के बीच स्पष्ट टकराव था। सर्वोच्च न्यायालय ने भावी प्रयोज्यता के सामान्य सिद्धांत पर अपवाद लागू करके ऐसा निर्णय लेने के पीछे कोई तर्क भी नहीं दिया।
गंडुरी कोटेश्वरम्मा और अन्य बनाम चकिरी यानिदी और अन्य (2011)
यह मामला इस कानूनी मुद्दे से जुड़ा था कि क्या संशोधित प्रावधान न्यायालय के समक्ष लंबित मामले पर लागू होंगे। इस मामले में, विचारण न्यायालय विभाजन और अलग कब्जे के मामले से निपट रहा था जिसमें अपीलकर्ता, मृतक की बेटी ने हिस्सों का दावा किया था। विचारण न्यायालय ने मामले में पहले ही एक प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी थी लेकिन अंतिम डिक्री का इंतजार था। इस बीच, 2005 का संशोधन लागू हुआ, जिसके कारण अपीलकर्ता ने अपने दावों में संशोधन किया और सहदायिक संपत्ति में समान हिस्सेदारी की मांग की। उसके दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उसे सहदायिक नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके पिता की मृत्यु संशोधन के लागू होने से पहले हो गई थी।
विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने फैसले को चुनौती दी कि विभाजन अंतिम नहीं था क्योंकि पक्षों द्वारा अंतिम डिक्री का इंतजार किया जा रहा था और इसलिए संशोधित अधिनियम की धारा 6 उसके लिए समान हिस्सों को सुनिश्चित करने के लिए मामले पर लागू होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभाजन के मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री निर्णय लेने की प्रक्रिया में केवल एक चरण है। जब तक अंतिम डिक्री पारित नहीं हो जाती, तब तक विभाजन को अंतिम नहीं माना जाता है। इसलिए, जब भी किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें अंतिम डिक्री पारित नहीं हुई है, तो ऐसी परिस्थिति पर विचार करना, यानी संशोधन करना और इसे अंतिम डिक्री में शामिल करना अदालत का कर्तव्य है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अंतिम डिक्री में बेटी को समान हिस्सेदारी दी जानी चाहिए।
यह देखते हुए कि कैसे इन तीन मामलों ने विभिन्न कानूनी मुद्दों को लेकर काफी भ्रम पैदा किया, सर्वोच्च न्यायालय के लिए विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के मामले में एक बार और सभी मुद्दों का पता लगाना महत्वपूर्ण था।
शामिल कानूनी मुद्दे
विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न मामलों पर भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए कानून के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना था:
- क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6, जिसे हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया है, को पूर्वव्यापी या भावी दृष्टि से लागू किया जा सकता है?
- क्या हिस्सों का निर्धारण करते समय प्रावधानों को लागू करने के लिए संशोधन के लागू होने के समय पिता और पुत्री दोनों का जीवित रहना आवश्यक है?
- क्या संशोधित प्रावधानों को संशोधन के प्रारंभ के दौरान न्यायालय में लंबित मामले पर लागू किया जा सकता है?
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इन मुद्दों पर विचार किया।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
यह निर्णय एक व्यापक निर्णय है जिसे सिद्धांतों की बेहतर समझ के लिए विभिन्न भागों में विभाजित किया जाना चाहिए।
पिछले/ लंबित निर्णयों का संदर्भ
सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 की व्याख्या के बारे में सवाल को सबसे पहले हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित एक बड़ी पीठ को भेजा था, जो प्रकाश बनाम फुलवती (2015) और दानम्मा बनाम अमर (2018) के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की दो खंडपीठों द्वारा लिए गए भ्रामक और परस्पर विरोधी विचारों के संबंध में था। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले अपने फैसले में इसी तरह के सवालों पर कई पिछले फैसलों का हवाला दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने लोकमणि एवं अन्य बनाम महादेवम्मा एवं अन्य (2018) के मामले का संज्ञान लिया, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना था कि 2005 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 6 को 17.6.1956 के दिन से अस्तित्व में माना जाना चाहिए, जो कि मूल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने की तिथि है। इसलिए, यह माना गया कि संशोधित प्रावधान प्रकृति में पूर्वव्यापी हैं और बेटियों को समान सहदायिक अधिकार प्रदान करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है। इसने कहा कि जब बेटियों को सहदायिक संपत्ति में अधिकारों से वंचित किया जाता है और मुकदमा लंबित है, तो इसे संशोधित प्रावधानों के आधार पर तय किया जाना चाहिए क्योंकि वे ऐसे मामलों पर लागू होंगे। कानून ने सहदायिक संपत्ति तक पहुंच के मामले में बेटों और बेटियों के बीच असमानता को दूर कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मौखिक विभाजन और अपंजीकृत विलेखों के माध्यम से किए गए विभाजन को “विभाजन” शब्द की परिभाषा से हटाया जाना है जो कि धारा 6(5) के स्पष्टीकरण में उल्लेखित हैं। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था।
इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने बालचंद्र बनाम श्रीमती पूनम एवं अन्य (2015) के मामले में उल्लेख किया कि 2005 के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा 6 के पूर्वव्यापी प्रभाव के बारे में प्रश्न पर विचार किया गया था। इस मामले में, पिता, जो हिंदू संयुक्त परिवार के मूल सहदायिक थे, 2005 के अधिनियम के लागू होने से पहले ही मर गए थे और तब से यह सवाल उठता है कि क्या बेटी को हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति का सहदायिक माना जा सकता है, भले ही उसके पिता संशोधन अधिनियम के लागू होने के दौरान जीवित न हों। इस मामले में निर्णय लंबित था और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिया जाना था।
सिस्टिया सारदा देवी बनाम उप्पलुरी हरि नारायण एवं अन्य (2018 ) विशेष अपील अनुमति (C) संख्या 38542/2016 के मामले में, प्रश्न इस तथ्य के संबंध में था कि जहां भी विभाजन के मामले में न्यायालय के समक्ष अंतिम डिक्री लंबित है, क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के संशोधित प्रावधानों के आधार पर सहदायिक संपत्ति पर बेटियों द्वारा निर्धारित हित को पुनः वितरित किया जा सकता है।

गिरिजाव्वा बनाम कुमार हनमंतगौड़ा एवं अन्य (2019) एसएलपी (सिविल) डायरी संख्या 3401/2019 के मामले में, प्रश्न यह था कि क्या 2005 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 6, संशोधन के लागू होने से पहले पिता की मृत्यु के मामले में भावी रूप से लागू होगी और क्या इस आधार पर बेटियों द्वारा दावा किए गए समान हिस्सों को अस्वीकार किया जा सकता है।
श्रीमती वी.एल जयलक्ष्मी बनाम वीएल बालकृष्ण एवं अन्य (2019) के मामले में, मुद्दा तब उठा जब 2001 में दायर एक मुकदमे में याचिकाकर्ता द्वारा मृतक पिता की पैतृक संपत्ति का विभाजन मांगा गया था, जिसमें विचारण न्यायालय ने सभी पक्षों को 1/7वां हिस्सा दिया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित किया गया और प्रकाश बनाम फुलवती (2015) के मामले के फैसले के आधार पर याचिकाकर्ता और अन्य बेटियों को 1/35वां हिस्सा दिया गया।
इंदुबाई बनाम यादवराव (2019) और बी.के वेंकटेश बनाम बी.के पद्मावती (2020) के मामले में बेटियों की सहदायिक के रूप में स्थिति और उन्हें समान हिस्सेदारी देने के संबंध में इसी तरह के सवाल उठाए गए थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि प्रकाश बनाम फुलवती (2015) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में, यह माना गया था कि 2005 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 6 का पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा और यह केवल उन मामलों पर लागू होगा जहां सहदायिक और उसकी बेटी दोनों संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के दौरान जीवित थे। खंडपीठ ने यह भी कहा था कि धारा 6(5) से जुड़े स्पष्टीकरण के लिए एक वैध विभाजन के पंजीकृत होने या अदालत की डिक्री के माध्यम से किए जाने की पूर्व शर्तों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की असंशोधित धारा 6 द्वारा प्रदान किए गए उत्तराधिकार के उद्घाटन पर किए गए वैधानिक काल्पनिक विभाजन पर लागू नहीं हो सकता है। खंडपीठ ने कहा था पंजीकरण की पूर्व शर्त उस विभाजन पर लागू नहीं होती जो कानून की प्रक्रिया द्वारा शासित होता है और इस प्रकार 2005 के अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 6 के प्रावधानों को खंडपीठ द्वारा भावी माना गया।
दानम्मा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि धारा 6 के संशोधित प्रावधान बेटियों को धारा 6 द्वारा प्रदत्त पूर्ण सहदायिक अधिकार प्रदान करते हैं और कोई भी सहदायिक, जिसमें बेटी भी शामिल है, सहदायिक संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकता है। इसने बेटियों को बेटों के बराबर हिस्सा दिया, फिर भी फुलवती मामले में इसने अनुपात को बरकरार रखा। इसे प्रकृति में अस्पष्ट माना गया है।
विभिन्न वकीलों के तर्क
इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अलग-अलग वकीलों द्वारा दी गई अलग-अलग दलीलों का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से राय मांगी थी और साथ ही इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक न्यायालय का मित्र (एमिकस क्यूरी) भी नियुक्त किया था।
न्यायालय के मित्र के तर्क
भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के महाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) श्री तुषार मेहता ने तर्क दिया कि संशोधन के पीछे की मंशा बेटियों को समान सहदायिक का दर्जा प्रदान करना था ताकि वे बेटों के साथ समानता हासिल कर सकें। सहदायिक संपत्ति से बेटियों को बाहर रखना एक दमनकारी कार्य है जो भेदभाव का मार्ग प्रशस्त करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। भले ही 2005 का संशोधन अधिनियम प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अपने संचालन में पूर्वव्यापी है क्योंकि यह बेटियों को 2005 के अधिनियम के प्रारंभ से सहदायिक का हिस्सा बनने के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। सहदायिकता जन्म से प्राप्त होती है और इसलिए यह बेटी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बेटी को सहदायिक का दर्जा दिए जाने से 20 दिसंबर, 2004 से पहले निष्पादित विभाजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कि वह तारीख है जिस दिन विधेयक संसद के ऊपरी सदन में पेश किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि मिताक्षरा कानून न केवल महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है, बल्कि दमनकारी भी है। इसलिए, 5.9.2005 से, जो संशोधन के लागू होने की तिथि है, सभी बेटियों को जन्म से सहदायिक का दर्जा प्राप्त हुआ और उन्हें बेटों के समान अधिकार और दायित्व मिले।
उन्होंने तर्क दिया कि यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संशोधन के बाद उत्तरजीविता (सर्वाइवरशिप) के माध्यम से सहदायिकता का हस्तांतरण समाप्त कर दिया गया था और वर्तमान में हस्तांतरण बिना वसीयत के उत्तराधिकार या वसीयतनामा (टेस्टामेंटरी) उत्तराधिकार के माध्यम से होता है। प्रकाश बनाम फुलवती (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि यह तथ्य कि निर्णय में जीवित पिता से जीवित पुत्री को सहदायिक अधिकार प्राप्त करने की मांग की गई थी, जन्म से सहदायिकता के मूल विचार के खिलाफ है। 2005 के संशोधन की धारा 6(3) के अनुसार, पिता की मृत्यु केवल तभी महत्वपूर्ण होती है जब सहदायिक संपत्ति में उनके हित के उत्तराधिकार की बात आती है। सहदायिक की मृत्यु से सहदायिकता समाप्त नहीं होती है, बल्कि हितों का पता लगाने के लिए काल्पनिक विभाजन लाया जाता है। अंतिम विभाजन होने तक नए सहदायिक भी जन्म से जुड़ते हैं। इसलिए सहदायिक संपत्ति में हित तब तक जारी रहते हैं जब तक कि पूर्ण विभाजन नहीं हो जाता। जब धारा 6 में “सहदायिक की बेटी” वाक्यांश का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब “जीवित पिता की बेटी” नहीं होता है। अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी सहदायिक जो पारिवारिक समझौते या मौखिक विभाजन पर भरोसा करता है, उसे विश्वसनीय दस्तावेजों के रूप में वैध साक्ष्य के माध्यम से इसे साबित करना होगा।
विद्वान वरिष्ठ वकील/ न्यायमित्र श्री आर. वेंकटरमणी ने तर्क दिया कि फुलवती और दानम्मा के निर्णयों के बीच कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इन दोनों निर्णयों में कहा गया है कि धारा 6 की भावी प्रयोज्यता होनी चाहिए क्योंकि संशोधन प्रकृति में भावी है। संशोधन के तहत बेटी को सहदायिक का दर्जा प्राप्त है, इसलिए नहीं कि वह संशोधन से पहले पैदा हुई थी। संशोधित धारा 6 की भाषा के अनुसार, पूर्वव्यापी प्रयोज्यता का कोई इरादा लागू नहीं होता है और भले ही इरादा समानता बनाने का हो, लेकिन यह पिछले लेन-देन को फिर से खोलने से संबंधित नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 6 का उद्देश्य किसी भी मौखिक विभाजन या पारिवारिक समझौते को फिर से खोलना नहीं है। यदि कानून संशोधन से पहले पैदा हुई बेटी को सहदायिक मानता है, तो इससे कानून के संचालन और कामकाज में कई तरह की उलझनें पैदा होंगी। विद्वान वकील के अनुसार, धारा 6 का दृष्टिकोण भविष्यवादी और दूरदर्शी है और इसलिए इसे उसी तरह से समझा जाना चाहिए।
विद्वान वरिष्ठ वकील और न्यायालय के मित्र श्री वी.वी.एस राव ने तर्क दिया कि प्रकाश बनाम फुलवती (2015) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पीछे के तर्क को मंगम्मल @ तुलसी और अन्य बनाम टीबी राजू और अन्य, (2018) के फैसले में बरकरार रखा गया है, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि संशोधित प्रावधानों के प्रारंभ होने की तिथि पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए जीवित सहदायिक की जीवित बेटी होनी चाहिए। जब कोई धारा 6(1)(a) को देखता है, तो यह एक बेटी को जन्म से सहदायिक का दर्जा प्रदान करता है और इस तरह की घोषणा के माध्यम से, एक बेटी सहदायिक का हिस्सा बन जाती है और इसलिए, पूर्वव्यापी या भावी प्रयोज्यता का सवाल नहीं उठना चाहिए क्योंकि भले ही बेटी 2005 से पहले या बाद में पैदा हुई हो, वह अभी भी जन्म से सहदायिक है। धारा 6 का विधायी इतिहास यह स्पष्ट करता है कि संसद का उद्देश्य बेटों और बेटियों के बीच संपत्ति में असमानता को खत्म करना था और यदि जीवित पिता और जीवित बेटी की आवश्यकता को बरकरार रखा जाता है तो यह इरादा विफल हो जाता है। विद्वान वकील के अनुसार, बेटी को सहदायिक का दर्जा देने के लिए आवश्यकता यह है कि 2005 के संशोधन के लागू होने की तिथि से एक सहदायिक होना चाहिए।
अपीलकर्ता द्वारा तर्क
विद्वान वकील श्री अमित पई ने तर्क दिया कि प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए व्याख्या के स्वर्णिम (गोल्डन) नियम को अपनाया जाना चाहिए। धारा 6 में संशोधन 1956 के मूल अधिनियम के अधिनियमन से संबंधित है। सहदायिक की मृत्यु पर एक काल्पनिक विभाजन वास्तविक विभाजन के बराबर नहीं माना जा सकता है, जो एक बार और सभी के लिए हिस्सों का फैसला करता है। उद्देश्यों और कारणों के कथनों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बेटियों को समानता के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, धारा 6 के प्रावधान पूरी तरह से प्रभावी होने चाहिए। फुलवती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सही नहीं है। प्रावधानों की भाषा जीवित पिता की जीवित बेटी को सहदायिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। किसी कानून में कोई अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ा या पढ़ा जा सकता है। न्यायालय के पास केवल त्रुटियों को सुधारने की शक्ति है। प्रावधान में सभी बेटियां शामिल हैं, भले ही उनके पिता संशोधन के प्रारंभ होने की तिथि पर जीवित हों या नहीं।

विद्वान वकील श्री समीर श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में कहीं भी सहदायिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सहदायिक को संयुक्त परिवार से भी छोटा माना गया है क्योंकि इसमें केवल वे लोग शामिल होते हैं जिन्होंने इसमें जन्म लिया है या सहदायिक संपत्ति में दावा प्राप्त किया है और इसलिए वे जब चाहें तब विभाजन की मांग कर सकते हैं। बेटियाँ धारा 6(1) और 6(5) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन, हिस्सों की हकदार हैं। उत्तरजीविता की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान तरीके केवल वसीयतनामा या निर्वसीयत (इंटेस्टेट) उत्तराधिकार के माध्यम से हैं, जिसमें संशोधन अधिनियम के अधिनियमन से पहले एक हिंदू की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश बनाम फुलवती (2015) के मामले में पीठ द्वारा दिया गया निर्णय जो जीवित पिता की जीवित बेटी के सिद्धांत को आवश्यक बनाता है, बिल्कुल अस्पष्ट है और कानून की नज़र में इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। सहदायिक स्थिति जन्म से दी जाती है और उस नियम का एकमात्र संभावित अपवाद गोद लेना हो सकता है।
विद्वान वकील सुश्री अनघा एस. देसाई ने तर्क दिया कि धारा 6 दिनांक 9 सितंबर, 2005 से हिंदू संयुक्त परिवार के बेटों और बेटियों के बीच हितों की समानता बनाती है। धारा 6 में दिया गया कथन कि सहदायिक की बेटी के पास बेटे के समान अधिकार और दायित्व होंगे, स्पष्ट और सुबोध (अनइक्विवोकल) है। जीवित पिता की आवश्यकता तर्कहीन है, क्योंकि यह प्रावधान के पूरे उद्देश्य को विफल कर देता है।
प्रतिवादियों के तर्क
विद्वान वकील श्री श्रीधर पोताराजू ने तर्क दिया कि प्रकाश बनाम फुलवती (2015) के निर्णय ने कानून की सही व्याख्या की है। उन्होंने तर्क दिया कि विवाहित बेटियों को उनके पिता के संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है और यह तथ्य कि उन्हें वर्ग I वारिस के रूप में माना जाता था, उन्हें उनके पिता के संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं बनाता है। विद्वान वकील के अनुसार, हिंदू सहदायिक हिंदू संयुक्त परिवार की तुलना में एक छोटा निकाय है। सहदायिक की बेटी का मतलब जीवित सहदायिक की बेटी से है। वैधानिक विभाजन की स्थिति में, स्थिति की संयुक्तता का विच्छेद (सीवरेंस) और हिस्सों का निपटान परिकल्पित है।
उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन से पहले दी गई उत्तरजीविता द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को संशोधित प्रावधानों द्वारा नहीं छीना जा सकता। धारा 6 को उसके संशोधित रूप में उस बेटी पर लागू नहीं किया जा सकता जिसका पिता संशोधन की शुरूआत के समय जीवित नहीं था। प्रारंभिक डिक्री के मामले में, उन्होंने तर्क दिया कि प्रारंभिक डिक्री का उपयोग पक्षों के हिस्सों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है और जब व्यक्तिगत हिस्सों का निर्धारण प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से पक्षों को आवंटित किया जाता है, तो इसे अंतिम माना जाता है। प्रारंभिक डिक्री के बाद उठाए जाने वाले एकमात्र कदम को पारित प्रारंभिक डिक्री के अनुसार परिधि (मेट्स) और सीमाओं के माध्यम से हिस्सों का आबंटन करना था।
इन सभी कारकों पर विचार करते हुए, उन्होंने अपने तर्कों का सारांश यह कहते हुए दिया कि धारा 6 का प्रभाव इसकी प्रयोज्यता में भावी होना चाहिए।
सहदायिक और संयुक्त हिंदू परिवार
सहदायिक और हिंदू संयुक्त परिवार की विशेषताओं के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि:
- हिंदू संयुक्त परिवार की तुलना में सहदायिक एक छोटा निकाय है। जबकि संयुक्त परिवार में सभी वंशज और उनकी पत्नियाँ और अविवाहित बेटियाँ शामिल होती हैं, लेकिन संपत्ति के बंटवारे के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
- सहदायिक में केवल एक प्रस्तावक (प्रोपोसीट्स) और तीन वंशज शामिल होते हैं। 2005 से पहले, इसमें बेटे, पोते और परपोते शामिल थे। इसलिए सहदायिक की संपत्ति वह होती है जो पिता, दादा या परदादा से विरासत में मिलती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सहदायिक उत्तराधिकारियों को जन्म से या गोद लेने से अधिकार प्राप्त होते हैं। पहले, महिला सहदायिक नहीं थी, बल्कि संयुक्त परिवार का हिस्सा थी। संशोधन ने बेटों की तरह ही जन्म से बेटियों के सहदायिक अधिकारों को मान्यता दी। केवल सहदायिक को ही बंटवारे की मांग करने का अधिकार है।
सहदायिकता का गठन
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सहदायिकता सहदायिकों के साझा स्वामित्व पर आधारित है। अविभाजित सहदायिकता में, हिस्से अनिश्चित होते हैं। हिस्से की सीमा पर कोई सटीकता नहीं है। हिस्से में उतार-चढ़ाव होता रहता है क्योंकि यह परिवार में मृत्यु या जन्म पर निर्भर करता है।
- माननीय न्यायालय ने सुनील कुमार एवं अन्य बनाम राम प्रकाश एवं अन्य (1988) के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें यह चर्चा की गई थी कि एक हिंदू संयुक्त परिवार सपिंडशिप के सिद्धांतों से बंधा होता है जो परिवार की संस्था के लिए आवश्यक हैं। सहदायिक में केवल वे लोग शामिल होते हैं जिनका संपत्ति में हित होता है और वे विभाजन को लागू कर सकते हैं और जन्म से स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।
- इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने शीला देवी एवं अन्य बनाम लाल चंद एवं अन्य (2006) में उल्लेख किया कि जब भी किसी सहदायिक की संपत्ति अस्थायी रूप से किसी अकेले व्यक्ति के हाथों में चली जाती है, तो वह उसकी संपत्ति बन जाती है, लेकिन एक बार बेटा पैदा होने पर सहदायिक फिर से जीवित हो जाता है। धर्म शामराव अगालावे बनाम पांडुरंग मिरगु अगालावे एवं अन्य (1988) में भी इसी तरह की टिप्पणियां की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त परिवार की संपत्ति एक जीवित सहदायिक के हाथों में होने के बाद भी अपना चरित्र बनाए रखती है, लेकिन एक बार बेटा पैदा होने या गोद लेने के बाद, सहदायिक जीवित रहता है।
- मद्रास के संपदा शुल्क नियंत्रक बनाम अल्लादी कुप्पुस्वामी (1969 ) के मामले में हिंदू सहदायिक की कुछ विशेषताओं को मान्यता दी गई। वे सहदायिक से तीसरी पीढ़ी तक के सीधे पुरुष वंशज होते हैं, सदस्यों को बंटवारे की मांग करने का अधिकार होता है, बंटवारे तक, प्रत्येक सदस्य के पास संयुक्त रूप से पूरी संपत्ति का स्वामित्व होता है, संपत्ति पर कब्ज़ा और उससे लाभ प्राप्त करना आपसी होता है, सभी सहदायिकों की सहमति के बिना संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं होता है, मृतक का हित मृत्यु पर समाप्त हो जाता है और संपत्ति में मिल जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, सहदायिकता व्यक्तिगत कानून का निर्माण है और इसलिए इसे पुनर्मिलन के मामले को छोड़कर पक्षों की मिलीभगत से नहीं बनाया जा सकता है। यह काफी हद तक एक निगमित निकाय या एक पारिवारिक संस्था है। सहदायिकता के समूह के बाहर, अन्य लोग हैं जो संयुक्त परिवार बनाते हैं। सहदायिकता की महत्वपूर्ण विशेषता समग्र स्वामित्व और हिस्सों में उतार-चढ़ाव है।
- वल्लिकन्नु बनाम आर. सिंगापेरुमल और अन्य (2005) में, यह दोहराया गया था कि सहदायिक में, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से समय-समय पर सहदायिक की मृत्यु या जन्म के आधार पर उतार-चढ़ाव करते हैं। संयुक्त परिवार के किसी भी व्यक्तिगत सदस्य को, जब तक यह बना रहे, अपने सटीक हिस्सों का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। सहदायिक के पास: “जन्म से अधिकार, उत्तरजीविता का अधिकार, विभाजन का अधिकार, संयुक्त कब्जे और आनंद का अधिकार, अनधिकृत कार्यों को रोकने का अधिकार, अलगाव (एलिनिएशन) का अधिकार, खातों का अधिकार और स्वयं अधिग्रहण करने का अधिकार है।”
- रोहित चौहान बनाम सुरिंदर सिंह एवं अन्य (2013) में यह माना गया कि सहदायिक वह व्यक्ति होता है जिसका उत्तराधिकार और पारस्परिक पूर्वज की संपत्ति तक पहुँच के मामले में सहदायिक के अन्य सदस्यों के साथ समान दावा होता है। सहदायिक के पास सहदायिक संपत्ति में केवल अविभाजित हित होता है और उसका कोई निश्चित हिस्सा नहीं होता।
- कटामा नचियार बनाम श्रीमत राजा मूत्तू विजया रागानाधा बोधा गोरो स्वामी पेरिया ओडया टावर (1863) के मामले में, यह माना गया कि वास्तविक विभाजन से सहदायिक को एक निश्चित हिस्से का हकदार बनाया जाता है। वास्तविक विभाजन तक, हित अविभाजित रहता है।
- भगवंत पी. सुलाखे बनाम दिगंबर गोपाल सुलाखे एवं अन्य (1986) में , यह माना गया कि संयुक्त परिवार की स्थिति के विच्छेद मात्र से सहदायिक संपत्ति में सहदायिक या सामान्य अविभाजित हित समाप्त नहीं होता है जब तक कि वास्तविक विभाजन न हो जाए।
- शंकरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम एम. प्रभाकर एवं अन्य (2011) में, यह माना गया कि सहदायिक संयुक्त स्वामित्व से बंधा होता है और संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए दायर किया गया मुकदमा सभी संयुक्त-मालिकों के लाभ के लिए होता है। सह-स्वामित्व केवल वास्तविक विभाजन और बंटवारा होने पर ही समाप्त होता है।

इन मामलों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सहदायिक तब तक अविभाजित रहता है जब तक वास्तविक विभाजन नहीं हो जाता। हिस्सों का अंतिम निर्धारण वास्तविक विभाजन के माध्यम से होता है, न कि काल्पनिक विभाजन के माध्यम से। वास्तविक विभाजन तक, हिस्से अविभाजित रहते हैं।
अबाधित और बाधित विरासत
सर्वोच्च न्यायालय ने अबाधित और बाधित विरासत की अवधारणाओं और इतिहास का उल्लेख करना आवश्यक समझा। इसने उन अवधारणाओं पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:
मिताक्षरा सहदायिक में दो प्रकार की विरासत होती है। अबाधित विरासत को “अप्रतिबंध दया” और बाधित विरासत को “सप्रतिबंध दया” भी कहा जाता है । जब भी जन्म के आधार पर कोई अधिकार बनाया जाता है, उसे अबाधित विरासत के रूप में जाना जाता है। अबाधित विरासत में, जन्म के समय होने वाला अधिकार पुरुष पूर्वजों की संपत्ति से अर्जित किया जाता है। ऐसी स्थिति में जहां सहदायिक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी को छोड़े मर जाता है, तो हित जन्म से अर्जित नहीं होता है, बल्कि पुरुष वंशज न होने के कारण होता है और ऐसा अधिकार बाधित विरासत होता है। इसे बाधित इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकार का निर्माण मालिक के जीवन से प्रभावित या बाधित होता है। धारा 6 के तहत केवल मृत्यु के बाद ही बाधित विरासत होती है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह अधिकार मालिक की मृत्यु पर निर्भर नहीं करता है और इसलिए धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार 9.9.2005 को सहदायिक पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है।
1956 के अधिनियम की धारा 6
सबसे विवादास्पद प्रावधान की व्याख्या की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि धारा 6 हिंदू संयुक्त परिवार की सहदायिक संपत्ति में अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित है, जो मिताक्षरा कानूनी प्रणाली द्वारा शासित है। प्रावधान के मूल संस्करण (वर्जन) ने मिताक्षरा सहदायिक संपत्ति पर उत्तराधिकार के नियम के प्रयोज्यता को अस्वीकार कर दिया और कहा कि 1956 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद मरने वाले सहदायिक पुरुष हिंदू का हित उत्तरजीविता के नियमों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और सहदायिक के जीवित सदस्यों पर हस्तांतरित किया जाएगा। अपवाद यह था कि यदि मृतक ने वर्ग 1 में एक जीवित महिला रिश्तेदार या उस वर्ग में एक पुरुष रिश्तेदार छोड़ा है जिसने महिला रिश्तेदार के माध्यम से दावा किया है, तो ऐसा हित मृतक सहदायिक के हिस्सों का पता लगाने के लिए वसीयतनामा या निर्वसीयत उत्तराधिकार द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। बाद में, 2005 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से धारा 6 के प्रावधान को प्रतिस्थापित करके इस लैंगिक भेदभाव को हटाने की परिकल्पना की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधन के बाद, बेटी को जन्म से बेटे की तरह ही सहदायिक का दर्जा दिया जाता है और उसे सहदायिक के समान ही अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। हालाँकि, धारा 6(1) में प्रावधान है कि धारा के प्रावधान 20.12.2004 से पहले किए गए किसी भी निपटान या अलगाव को अमान्य नहीं करेंगे। संशोधन यह स्पष्ट करता है कि इसका उद्देश्य भेदभाव को दूर करना है। कई राज्यों में बेटियों को समान अधिकार देने के लिए विभिन्न राज्य संशोधन भी किए गए।
संशोधित प्रावधानों में यह प्रावधान है कि संशोधन के लागू होने की तिथि से ही बेटी को बेटे की तरह ही सहदायिक का अधिकार प्राप्त होगा। धारा 6(1)(a) मिताक्षरा सहदायिक में परिकल्पित अबाधित विरासत की अवधारणाओं से संबंधित है। धारा 6(1)(b) बेटियों को बेटों के समान ही अधिकार प्रदान करती है। भले ही संशोधन के लागू होने की तिथि से अधिकारों का दावा किया जा सकता है, लेकिन प्रावधान प्रकृति में पूर्वव्यापी हैं और उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। प्रावधानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ पूर्ववर्ती घटना पर आधारित हैं।
उपरोक्त तर्क के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जबकि एक भावी क़ानून अधिनियमन की तिथि से लागू होता है और नए अधिकारों की कल्पना करता है, तब एक पूर्वव्यापी क़ानून पीछे की ओर कार्य करता है और मौजूदा कानूनों के माध्यम से प्राप्त निहित अधिकारों को छीन लेता है या प्रभावित करता है। दूसरी ओर, एक पूर्वव्यापी क़ानून पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं होता है, बल्कि भविष्य में संचालित होता है, लेकिन इसका संचालन पहले उत्पन्न हुए चरित्र या स्थिति पर आधारित होता है। चूँकि प्रावधान जन्म से अधिकार प्रदान करते हैं, जो एक पूर्ववर्ती घटना है, इसलिए प्रावधान पूर्वव्यापी है।
भ्रम की स्थिति को दूर करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9.9.2005 के बाद सहदायिक की मृत्यु के मामले में, उत्तराधिकार उत्तरजीविता द्वारा शासित नहीं होता है, बल्कि धारा 6(3)(1) के अनुसार शासित होता है। धारा 6(1) और (5) का प्रावधान 20.12.2004 से पहले किसी भी विभाजन प्रभाव को बचाता है। हालाँकि, स्पष्टीकरण में कहा गया है कि विभाजन को तभी मान्यता दी जाती है जब यह विभाजन के पंजीकृत विलेख या न्यायालय के आदेश के माध्यम से किया जाता है।
प्रावधानों में अबाधित विरासत में परिकल्पित असंहिताबद्ध (अनकोडिफाइड) हिंदू कानून की अवधारणा को आकार दिया गया है और इसलिए, बेटी को सहदायिक का अधिकार प्राप्त करने के लिए उसके पिता का संशोधन की तिथि पर जीवित होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बेटी अधिनियम से पहले या बाद में जन्म लेकर बेटे के रूप में सहदायिक बन जाती है। इन अधिकारों का दावा केवल संशोधन की तिथि यानी 9.9.2005 से ही किया जा सकता है, जबकि 20.12.2004 से पहले किए गए विभाजन को बरकरार रखा जा सकता है।
बेटियों के अधिकारों के विस्तार का प्रभाव
2005 के संशोधन से पहले धारा 6 के प्रावधान के अनुसार, जब कोई सहदायिक व्यक्ति मर जाता है, और अपने पीछे वर्ग 1 के वारिस की महिला रिश्तेदार या ऐसे वर्ग 1 की महिला वारिस के माध्यम से दावा करने वाला पुरुष वंशज छोड़ जाता है, तो बेटी वारिसों में से एक होती है। धारा 6, अपने संशोधित संस्करण में, सहदायिक व्यक्ति के अस्तित्व को पूर्वकल्पित करती है। यह केवल बेटी के अधिकारों को बढ़ाता है और अन्य सभी रिश्तेदारों के अधिकार समान और अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि प्रावधान में उल्लेख किया गया है।
इस अवधारणा पर, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी भी सहदायिक के पास संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा नहीं होता है। नए सहदायिकों की मृत्यु या जन्म के आधार पर हिस्सों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। यह सिद्धांत धारा 6 के प्रावधानों में निहित है। काल्पनिक या विचारमूलक (नोशनल) विभाजन से सहदायिकता में कोई व्यवधान नहीं होता है। काल्पनिक विभाजन का उपयोग केवल मृतक सहदायिक के हिस्सों का पता लगाने के लिए किया जाता है जो वास्तविक विभाजन होने पर उसे सौंपे जाते है।
सहदायिक संपत्ति में अधिकारों का अधिग्रहण
संपत्ति में हिस्सेदारी जन्म से अर्जित होती है और सहदायिक की मृत्यु पर हस्तांतरण होता है। पहले, हस्तांतरण उत्तरजीविता द्वारा शासित होता था, लेकिन 1956 के बाद, महिलाएं भी असंशोधित धारा 6 के प्रावधान में उल्लिखित स्थितियों/आकस्मिकताओं में उत्तराधिकार प्राप्त कर सकती थीं। काल्पनिक कल्पना ने बेटियों को सहदायिक माना। सहदायिकता जन्म या गोद लेने के आधार पर होती है, न कि हित के हस्तांतरण से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि एक जीवित पिता एक जीवित बेटी को सहदायिक अधिकार देता है क्योंकि सहदायिकता का अधिकार पिता या किसी अन्य सहदायिक की मृत्यु से प्राप्त नहीं होता है। यह केवल जन्म से शासित होता है।
यह तर्क दिया गया कि यदि संसद का इरादा 2005 से पहले जन्मों की घटनाओं का उल्लेख करना था, तो उसने प्रावधान को अधिनियमित नहीं किया होगा। जब प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाता है, जब जन्म से सहदायिक की बेटी को अधिकार प्रदान किया जाता है, उसी तरह जैसे बेटों को अधिकार प्राप्त होता हैं, तो 20.12.2004 से पहले के पूर्व निपटान या अलगाव को बचाना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, भले ही अधिकार जन्म से प्राप्त होता है, लेकिन इसे केवल 9.9.2005 से ही लागू किया जा सकता है। प्रावधान केवल पिछले लेन-देन को किसी भी तरह के अमान्य होने से बचाता है।
यह तर्क दिया गया था कि यदि किसी बेटी को जन्म से सहदायिक अधिकार दिए जाते हैं और उसे अतीत में किसी बिंदु से सहदायिक माना जाता है, तो यह कानून के सामान्य संचालन को प्रभावित करेगा और कई अनिश्चितताओं को जन्म देगा। सर्वोच्च न्यायालय की राय में, ऐसी कोई अनिश्चितता उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि धारा 6 मिताक्षरा सहदायिक कानूनों के सिद्धांतों द्वारा शासित होती है, जो जीवित सहदायिकों के हिस्सों को तब तक अनिश्चित बनाती है जब तक वास्तविक विभाजन नहीं हो जाता। किसी भी पक्ष के पास कोई निश्चित हिस्सा नहीं है और वास्तविक विभाजन होने तक हित अविभाजित रहता है। पूर्व तिथि से अधिकारों का सम्मान अतीत को पुनर्जीवित करना नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती घटना को भविष्य में अधिकारों के सम्मान के तरीके के रूप में मान्यता देना है। ऐसा कार्य निश्चित रूप से सहदायिक के आकार को बढ़ाता है और सहदायिक को बेटियों के साथ असमान व्यवहार करने से रोकता है।

प्रकाश बनाम फुलवती (2015) में, पिता की मृत्यु 1988 में हो गई और बेटियों ने 1992 में विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया, जिसे 2007 में खारिज कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने संशोधित प्रावधान को लागू किया और बेटियों के साथ समान व्यवहार किया। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान पूर्वव्यापी नहीं है। पंजीकरण के माध्यम से किए जाने वाले विभाजन की आवश्यकता को धारा 6 के असंशोधित प्रावधान के अनुसार उत्तराधिकार की शुरुआत पर माने गए या काल्पनिक विभाजन पर कोई प्रभाव नहीं डालने वाला माना गया। यह माना गया कि संशोधन द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल 9.9.2005 तक जीवित पिता की जीवित बेटियों पर लागू होते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के अपने फैसले में कहा कि हो सकता है कि पिछले फैसले में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया हो कि सहदायिक कैसे बनता है। सहदायिक बनने या सहदायिक को बनाने के लिए सहदायिक का जीवित रहना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ निश्चित डिग्री के भीतर जन्म ही एकमात्र प्रासंगिक कारक है। उत्तरजीविता केवल उत्तराधिकार का एक तरीका है और सहदायिक बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, जीवित सहदायिक की आवश्यकता को खारिज कर दिया गया।
मंगम्मल बनाम टी.बी राजू एवं अन्य (2018) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 में तमिलनाडु राज्य में लागू प्रावधानों पर विचार किया, जिसे 25.03.1989 से प्रभावी किया गया और धारा 29A को जोड़ा गया, जिसे उत्तरजीविता द्वारा उत्तराधिकार के संबंध में सही माना गया। धारा 29A ने बेटियों को सहदायिक संपत्ति में बेटों के समान हित प्रदान किए। प्रावधान कुछ हद तक समान थे, सिवाय 29A(iv) के जिसमें विवाहित बेटियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। 1989 संशोधन की शुरुआत की तिथि से पहले विवाह करने वाली बेटियों पर ये प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। 2005 के संशोधन अधिनियम की धारा 6 में विवाहित बेटियों के खिलाफ भेदभाव को भी समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फूलवती और दानम्मा के फैसले को यह कहते हुए बरकरार रखा कि एक जीवित बेटी के लिए पिता का जीवित होना आवश्यक है। ऐसा विचार स्वीकार्य नहीं है।
अमर बनाम दानम्मा (2018) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश बनाम फूलवती (2015) के फैसले को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अमर बनाम दानम्मा (2018) मामले में की गई कुछ टिप्पणियाँ स्वीकार्य हैं, लेकिन प्रकाश बनाम फूलवती (2015) के फैसले को मंजूरी देने वाले हिस्से को बरकरार नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, जीवित सहदायिक की जीवित बेटी की अवधारणा के संबंध में फुलवती और दानम्मा के फैसलों के बीच स्पष्ट टकराव है।
विभाजन और वैधानिक कल्पना का प्रभाव
विभाजन के सिद्धांतों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभाजन की मांग करने के अधिकार को सहदायिक की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना गया है। इसलिए, सहदायिक के मूल अधिकारों में से एक विभाजन का दावा करना है। 9.9.2005 से बेटी के सहदायिक बन जाने से वैधानिक प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह देखते हुए कि बेटी के अधिकार अब बेटे के समान ही हैं, वह भी विभाजन का दावा कर सकती है। सहदायिक की विधवा भी बराबर हिस्से की हकदार है और उस अधिकार को छीना नहीं जा सकता।
सर्वोच्च न्यायालय ने हरदेव राय बनाम शकुंतला देवी एवं अन्य (2008) के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया था कि जब भी विभाजन का इरादा सामने आता है, तो प्रत्येक सहदायिक के हिस्से स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाते हैं और एक बार यह निर्धारित हो जाने के बाद, प्रत्येक सहदायिक अपने हिस्से का मालिक बन जाता है और उसे अलग संपत्ति के रूप में अलग करने का अधिकार होता है। सहदायिक संपत्ति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अंतिम विभाजन के बिना, केवल अविभाजित हिस्सों को विशिष्ट संपत्ति या संयुक्त कब्जे को प्रभावित किए बिना बेचा जा सकता है।
इसी तरह, मुसम्मत गिरजा बाई बनाम सदाशिव धुंडीराज (1916) में , यह माना गया कि विभाजन के लिए मुकदमा दायर करना एक व्यक्ति के अपने संबंधों को तोड़ने और उस तारीख से संयुक्त परिवार से अलग होने के इरादे का स्पष्ट प्रतिबिंब है। यहाँ एक सावधानी यह भी जोड़ी गई कि यदि बाद के चरण में कानून कोई अधिकार प्रदान करता है, या कोई घटना घटती है, तो ऐसी घटना के प्रभाव को प्रारंभिक डिक्री के साथ पता लगाना होगा।
आई.टी अधिकारी, कालीकट बनाम श्रीमती एन.के सरदा थम्पट्टी (1991) में, यह माना गया कि एक बार प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने के बाद, यह अपने आप में विभाजन का गठन नहीं करता है। वास्तविक विभाजन केवल अंतिम डिक्री के पारित होने के बाद ही होता है। ए.स नारायण रेड्डी और अन्य बनाम ए.स साई रेड्डी (1990) के मामले में, यह माना गया कि जब तक प्रत्येक सहदायिक को अलग-अलग संपत्तियों के अलग-अलग कब्जे में रखने के लिए अंतिम डिक्री पारित नहीं की जाती, तब तक विभाजन पूरा नहीं होता। एक प्रारंभिक डिक्री वास्तविक विभाजन बनाने में सक्षम नहीं है। अंतिम डिक्री के लंबित रहने के दौरान, बीच-बीच में होने वाली घटनाओं के कारण हिस्सों में बदलाव हो सकता है और इसलिए एक प्रारंभिक डिक्री अपरिवर्तनीय नहीं है।
प्रेमा बनाम नांजे गौड़ा एवं अन्य (2011) के मामले में, कर्नाटक राज्य द्वारा राज्य संशोधन के माध्यम से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में धारा 6A डाली गई थी। इस धारा ने महिलाओं को समान अधिकार दिए। संशोधन पर एक लंबित मुकदमे में विचार किया गया जहां केवल एक प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी और यह माना गया था कि संशोधन के प्रावधानों के आधार पर अंतिम डिक्री को बदला जा सकता है। यदि प्रारंभिक डिक्री पारित करने के बाद हिस्सों में वृद्धि या कमी होती है, तो न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री का मसौदा तैयार करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। गंडूरी कोटेश्वरम्मा एवं अन्य बनाम चाकिरी यानाडी एवं अन्य (2005) के मामले में l, यह निर्णय लिया गया था कि प्रारंभिक डिक्री को संशोधित किया जा सकता है क्योंकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, धारा 6 को 2005 के संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था प्रारंभिक डिक्री केवल पक्षों के अधिकारों और दावों का पता लगाती है, लेकिन विभाजन के मुकदमे का निपटारा तब तक नहीं किया जाता जब तक कि अंतिम डिक्री पारित न हो जाए, जो परिधि और सीमाओं के माध्यम से विभाजन को प्रभावी बनाती है। यदि प्रारंभिक डिक्री पारित होने के बाद, कोई भी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें ध्यान में रखे। न्यायालय को एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री पारित करने से कोई नहीं रोकता है।
लक्ष्मी नारायण गुइन एवं अन्य बनाम निरंजन मोडक (1985) के मामले में यह माना गया कि यदि अपील के लंबित रहने के दौरान पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो मामले पर अपना अंतिम निर्णय देते समय न्यायालय को इसे ध्यान में रखना चाहिए। अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने के बाद भी परिवर्तनों को प्रभावी कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार सहदायिक की स्थिति सहदायिक के जन्म या मृत्यु के साथ बदल जाती है, तो वास्तविक विभाजन के समय हिस्सों का पता लगाना होगा। हिस्सों का निर्धारण बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। स्थिति का विच्छेद वैधानिक प्रावधानों और बाद की घटनाओं के माध्यम से किए गए परिवर्तनों को लागू करने के रास्ते में नहीं आ सकता है। विभाजन की वैधानिक कल्पना या जिसे काल्पनिक विभाजन कहा जाता है, वह वास्तविक विभाजन से बहुत अलग है।
इसने आगे स्पष्ट किया कि काल्पनिक विभाजन संयुक्त परिवार या सहदायिकता को समाप्त नहीं करता है। इसलिए, मुकदमा शुरू करके स्थिति को अलग करने मात्र से विभाजन नहीं होता है और एक बार अंतिम डिक्री पारित हो जाने के बाद ही विभाजन को अंतिम माना जा सकता है। अंतिम डिक्री की प्रतीक्षा करते हुए, न्यायालय को परिस्थितियों और घटनाओं में हर तरह के बदलाव को ध्यान में रखना होगा। एक कानूनी कल्पना केवल उस उद्देश्य के लिए होती है जो वह पूरा करती है और इसे उद्देश्य से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
ग्यारसी राय एवं अन्य बनाम धनसुख लाल एवं अन्य (1965) के मामले में, यह माना गया कि मृतक सहदायिक के हिस्से का पता लगाने के लिए सभी सहदायिकों के हिस्सों की गणना की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में, विभाजन मान लिया जाता है और अंततः तभी प्रभावी होता है जब आवंटन का प्रश्न उठता है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना नहीं था कि एक माना या काल्पनिक विभाजन एक संयुक्त परिवार या सहदायिक को समाप्त कर सकता है।
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, पिछले सभी निर्णयों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि जब अधिकार बाद में प्रदान किए जाते हैं, तो प्रारंभिक डिक्री में संशोधन किया जा सकता है और कानून द्वारा दिए गए लाभ को ध्यान में रखना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 6 के प्रावधान के वैधानिक कल्पना के प्रभाव को खारिज कर दिया, जैसा कि फुलवती और दानम्मा मामलों में चर्चा की गई थी। एक बेटी जन्म से ही सहदायिक अधिकारों को प्रभावित करती है और वे संशोधन के प्रारंभ होने की तारीख से प्रभावी होते हैं।
धारा 6(5) का संदर्भ
धारा 6(5) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि विभाजन का अर्थ है कोई भी विभाजन जो न्यायालय के आदेश या पंजीकृत विभाजन विलेख के माध्यम से प्रभावित होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस स्पष्टीकरण का मूल संशोधन विधेयक में कोई स्थान नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया था। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, विभाजन का अर्थ पंजीकृत विभाजन विलेख या न्यायालय के आदेश द्वारा किया जाना होगा। जब भी विभाजन मौखिक होता है, तो इसे साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। शुरू में, विधायिका मौखिक विभाजन को भी मान्यता देना चाहती थी, लेकिन इससे दिखावटी या फर्जी लेन-देन हो सकता था।

धारा 6 के संशोधित संस्करण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेटियों को सहदायिक संपत्ति पर उनके दावों से वंचित न किया जाए। मौखिक विभाजन के धोखाधड़ीपूर्ण बचाव या विभाजन के अपंजीकृत ज्ञापन (मेमो) पर दिखावटी विभाजन का दावा करने से वह उद्देश्य विफल हो जाता है। न्यायालय को इस तथ्य से सावधान रहना चाहिए कि मौखिक विभाजन का दावा धोखे से, धोखाधड़ी के लिए एक ठोस प्रयास के माध्यम से किया जा सकता है या विभाजन के ज्ञापन पर आधारित हो सकता है जो पंजीकृत नहीं है। इस तरह के विभाजन को धारा 6(5) के तहत मान्यता नहीं दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का उद्देश्य विफल न हो।
काले एवं अन्य बनाम उप निदेशक, चकबंदी एवं अन्य (1976) के मामले में, यह माना गया था कि विभाजन के लिए पारिवारिक व्यवस्था के मामले में, सदस्यों के बीच हिस्सों के निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण के माध्यम से पारिवारिक विवादों या प्रतिद्वंद्वी दावों को हल करने के लिए समझौता सद्भाव के साथ किया जाना चाहिए। इसे बिना किसी दबाव, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव के स्वेच्छा से किया जाना चाहिए। यह मौखिक हो सकता है और इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं हो सकती है। न्यायालय को जानकारी दर्ज करने या प्रदान करने के उद्देश्य से पारिवारिक व्यवस्था के बाद तैयार किया गया मात्र ज्ञापन अचल संपत्तियों में किसी भी अधिकार को समाप्त नहीं करता है। चिंतामणि अम्मल बनाम नंदगोपाल गौंडर, (2007) में यह माना गया कि विभाजन की दलील को कानून के तहत प्रमाणित किया जाना चाहिए और हमेशा संयुक्तता की धारणा होती है। सह-हिस्सों द्वारा अलग-अलग कब्जा विभाजन की धारणा नहीं है।
पहले मौखिक बंटवारा स्वीकार्य था और बंटवारे का दावा करने वाले व्यक्ति पर सबूत का भार रहता था। समानता की समाप्ति को बंटवारे का वैध सबूत नहीं माना जाता था। संयुक्त परिवार के सदस्य सुविधा के लिए भोजन या निवास के आधार पर अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे संयुक्त परिवार या सहदायिकता समाप्त नहीं होती। यह एक सामान्य धारणा है कि प्रत्येक हिंदू परिवार संयुक्त होता है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। यहां तक कि जब एक सहदायिक अलग हो जाता है, तो दूसरा संयुक्त रहता है। बंटवारे का मुकदमा दायर करने की तारीख से स्थिति का विच्छेद हो सकता है, लेकिन इस तरह के विच्छेद के परिणामों को सुनिश्चित करने और अंतिम डिक्री में निश्चित हिस्सों को आवंटित करने के लिए डिक्री आवश्यक है। अंतिम डिक्री के लंबित रहने के दौरान होने वाले परिवर्तनों से निश्चित हिस्सों को बदला जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभाजन की एक विशेष परिभाषा की आवश्यकता है। प्रावधान का उद्देश्य दिखावटी बंटवारे के माध्यम से बेटी के अधिकारों को खतरे में डालना नहीं है। इसलिए, मौखिक विभाजन की दलील को अदालत द्वारा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसे दावा करने वाले व्यक्ति को दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से साबित करना होगा।
संक्षिप्त निर्णय
अंततः, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को बरकरार रखा:
- संशोधित धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को सहदायिक का दर्जा प्रदान किया गया है तथा उसे बेटे के समान अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे।
- 9.9.2005 से पहले पैदा हुई बेटी धारा 6(1) में प्रदत्त बचाव के साथ अपने अधिकारों का दावा कर सकती है, जो 20.12.2004 से पहले हुए विभाजन के किसी भी निपटान, अलगाव की रक्षा करती है।
- यह देखते हुए कि सहदायिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन के लागू होने की तिथि पर पिता जीवित हो।
- असंशोधित अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान में अधिनियमित विभाजन की वैधानिक कल्पना से सहदायिक का कोई वास्तविक विभाजन या विघटन नहीं हुआ। यह कल्पना केवल मृतक सहदायिक के हिस्सों का पता लगाने के उद्देश्य से थी और इसे उससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
- मौखिक विभाजन के बचाव को विधिवत पंजीकृत विलेख या न्यायालय के आदेश द्वारा किए गए विभाजन के क़ानून द्वारा अधिकृत तरीके के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। दुर्लभ मामलों में, विश्वसनीय दस्तावेजों द्वारा स्थापित मौखिक विभाजन के बचाव को न्यायालय के आदेश के समान ही स्वीकार किया जा सकता है।
- इसी प्रकार के मामलों पर विभिन्न न्यायालयों में लंबित सभी मुकदमों और अपीलों में कानूनी उलझन के कारण देरी हो गई थी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों का पालन करते हुए छह महीने के भीतर उन मुकदमों का निपटारा करने का आदेश दिया।
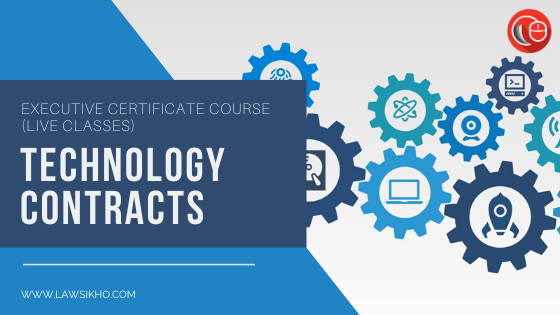
निष्कर्ष
इस मामले में निर्णय कानूनी चर्चा का एक विस्तृत और व्यापक हिस्सा है, जिसमें विभिन्न प्रावधानों, मिसालों और सिद्धांतों को शामिल किया गया है, ताकि किसी धारा की प्रयोज्यता के बारे में कानूनी भ्रम को अंततः सुलझाया जा सके। इस भ्रम का मूल रूप से कई बेटियों द्वारा किए गए संपत्ति पर समान दावों से वंचित होना या देरी करना था और इसलिए इसे एक बार और हमेशा के लिए सुलझाना महत्वपूर्ण था। यह निर्णय आने वाले वर्षों में महिलाओं के सहदायिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के साथ-साथ सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के संशोधित प्रावधान का क्या प्रभाव है?
इस प्रावधान को न तो भावी और न ही पूर्वव्यापी प्रकृति का माना गया। इसे पूर्वव्यापी घोषित किया गया क्योंकि इसका प्रभाव एक पूर्ववर्ती (एंटीसेडेंट) घटना पर निर्भर करता है, जो कि एक बेटी का जन्म है और इसलिए, जन्म से प्राप्त अधिकार और दावे एक पूर्ववर्ती घटना है, लेकिन संशोधन की तारीख से उनका प्रभाव शुरू होता है।
क्या सहदायिक बनने के लिए पुत्री के लिए यह आवश्यक है कि 2005 अधिनियम के लागू होने की तिथि पर उसके पिता जीवित हों?
नहीं, यह देखते हुए कि सहदायिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, सहदायिक अधिकार प्राप्त करने के लिए बेटी के लिए संशोधन की तिथि पर जीवित पिता का होना आवश्यक नहीं है।
मौखिक विभाजन का क्या प्रभाव है?
मौखिक विभाजन को तब तक वैध विभाजन नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि इसकी वास्तविकता को पुष्ट करने वाले मजबूत और पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य न हों।
विभाजन वास्तव में कब प्रभावित होता है?
विभाजन तभी पूरा होता है जब विभाजन के मुकदमे में न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की जाती है या पंजीकृत विभाजन विलेख के माध्यम से, जहाँ प्रत्येक सहदायिक के हिस्से निश्चित किए जाते हैं और फिर उनके अलग-अलग दावों के आधार पर उन्हें आवंटित किए जाते हैं। न्यायालय की प्रारंभिक डिक्री विभाजन को स्पष्ट नहीं करती है।
संदर्भ