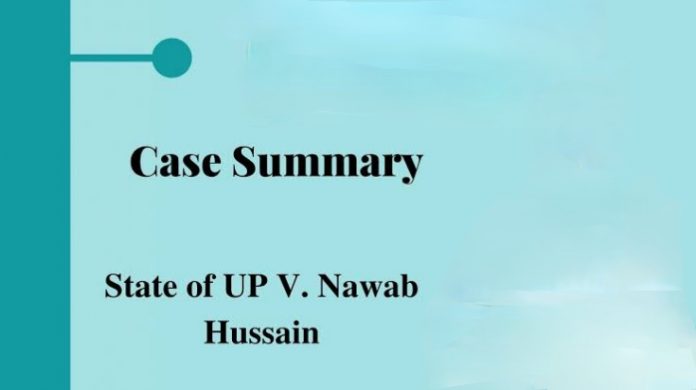यह लेख Nishimita Tah द्वारा लिखा गया है। यह उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन (1977) के ऐतिहासिक निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्यों, मुद्दों, विवादों और न्यायालय के निर्णय को विस्तार से शामिल किया गया है। इस लेख में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11, जो पूर्व-न्याय (रेस जुडिकाटा) से संबंधित है, पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
पूर्व-न्याय का नियम “नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईएडेम कॉसा” कहावत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि किसी को भी एक ही कारण और हित के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी), 1908 की धारा 11 एक ही प्रकृति के मुकदमों को दायर करने से मना करती है, जिसमें एक ही कारण और एक ही पक्ष के बीच हित के मुद्दे हों। यह धारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि एक बार जब कोई मामला सक्षम न्यायालय द्वारा तय और अंतिम रूप से तय कर दिया जाता है, तो पक्षों को उसी प्रकृति और हित का नया वाद दायर करके मामले को फिर से खोलने की अनुमति नहीं होती है। धारा 11 के तहत पूर्व-न्याय को सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक हित के साथ समाहित किया गया है। पूर्व-न्याय का सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है और उसी मुद्दे, कारण और हित से जुड़े मुकदमों को रोकता है, जिनकी सुनवाई पहले ही हो चुकी है और जहां सक्षम न्यायालय द्वारा पहले ही निर्णय दिया जा चुका है।
भारत के संविधान में दोहरे खतरे की अवधारणा शामिल है, जो अनुच्छेद 20(2) के तहत निहित मौलिक अधिकारों में से एक है। यह अनुच्छेद दोहरे खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है और “नेमो डेबेट बिस वेक्सारी” कहावत को मूर्त रूप देता है, जो एक सामान्य कानून नियम है जिसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार वाद नहीं चलाया जाना चाहिए।
वर्तमान मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत पूर्व-न्याय की अवधारणा और रिट याचिकाओं पर इसकी प्रयोज्यता (ऍप्लिकेबिलिटी) पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन (1977) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीपीसी की धारा 11 के तहत व्यक्त किए गए पूर्व-न्याय और रचनात्मक (कंस्ट्रक्टिव) पूर्व-न्याय के नियम के बीच एक सामान्य अंतर निर्दिष्ट किया। यह मामला भारतीय न्यायिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में चिह्नित है, जो सीपीसी के तहत पूर्व-न्याय की अवधारणा की प्रासंगिकता को उजागर करता है।
मामले का विवरण
मामले का नाम
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन
उद्धरण
1977 एआईआर 1680

याचिकाकर्ता का नाम
उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिवादी का नाम
नवाब हुसैन
मामले का प्रकार
सिविल अपील
न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
पीठ
न्यायमूर्ति पी.एन. शिंगल, न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.के. गोस्वामी
निर्णय की तिथि
04.04.1977
शामिल कानून
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 और भारत के संविधान का अनुच्छेद 311
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में प्रतिवादी नवाब हुसैन उत्तर प्रदेश राज्य के संवर्ग (कैडर) के तहत काम करने वाले पुलिस उपनिरीक्षक थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। इसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए। इन दोनों मामलों में की गई जांच के निष्कर्षों के आधार पर, प्रतिवादी को उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
प्रतिवादी ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई। उन्होंने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक (डिसिप्लिनरी) कार्यवाही में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने का उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई इस प्रकार अन्यायपूर्ण थी। हालांकि, इस रिट याचिका को भी खारिज कर दिया गया।
इसके बाद, उन्होंने सिविल न्यायाधीश की न्यायालय में एक दीवानी वाद दायर किया, जिसमें उनकी सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी गई। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था, और संविधान के अनुच्छेद 311(1) के प्रावधानों के तहत, डीआईजी को उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार नहीं था।
उत्तर प्रदेश राज्य ने इस वाद को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह वाद ‘पूर्व-न्याय’ के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, क्योंकि वर्तमान मामले से संबंधित सभी आधार विशेष अपील और रिट याचिका में उठाए जा चुके हैं या उठाए जाने चाहिए थे।
इस वाद को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। जिला न्यायाधीश ने भी अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा। प्रतिवादी ने दूसरी अपील दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया। इसके बाद यह अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंची।
उठाए गए मुद्दे
वर्तमान मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रिट आवेदनों पर लागू होता है, विशेष रूप से उन मुद्दों के संबंध में जिन्हें पहले उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं उठाया गया?
- क्या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में गुण-दोष के आधार पर उच्च न्यायालय का निर्णय, उसी मामले से संबंधित उन्हीं पक्षों के बीच एक बाद के नियमित वाद में पूर्व-न्याय का गठन करता है?
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता
- याचिकाकर्ताओं ने कई आधारों पर तर्क दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि प्रतिवादी द्वारा सिविल न्यायालय में दायर की गई याचिका पूर्व-न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित थी। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में सभी तर्क या तो विशेष अपील और रिट याचिका में उठाए गए थे या उठाए जाने चाहिए थे।
प्रतिवादी
- प्रतिवादी के पास मुख्य रूप से दो तर्क थे। सबसे पहले, उसने तर्क दिया कि उसे सेवा से बर्खास्त करना उचित नहीं था क्योंकि उसे आरोपों के खिलाफ बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।
- दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उनकी नियुक्ति पुलिस महानिरीक्षक द्वारा की गई थी, इसलिए केवल महानिरीक्षक ही उनकी नौकरी समाप्त करने के लिए अधिकृत थे। इस प्रकार, पुलिस के डीआईजी द्वारा जारी बर्खास्तगी का आदेश कानून के विरुद्ध था क्योंकि वह प्रतिवादी की सेवा समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (अथॉरिटी) नहीं थे।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन (1977) में चर्चित कानून
“पूर्व-न्याय” एक कानूनी वाक्यांश है जिसे आधुनिक कानूनी चर्चा में आमतौर पर “दावा निवारण” (क्लेम प्रेक्लुशन) के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह वाक्यांश कानूनी कार्यवाही में निर्णय के बाध्यकारी प्रभाव को दर्शाता है और यह गारंटी देता है कि पहले से ही सुलझाए गए विवादों को फिर से नहीं उठाया जा सकता है।
सीपीसी के अंतर्गत धारा 11
सीपीसी की धारा 11 में यह अभिव्यक्त किया गया है कि किसी न्यायालय को ऐसे वाद की सुनवाई नहीं करनी चाहिए जो किसी पूर्ववर्ती (फॉर्मर) वाद में सीधे तौर पर या काफी हद तक संबंधित हो या जिसका निर्णय उसी विषय-वस्तु पर उन्हीं पक्षों के बीच किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया हो, ताकि ऐसे मुद्दों की सुनवाई की जा सके जिन्हें उस न्यायालय द्वारा निश्चित और अंतिम रूप दिया जा चुका हो।

धारा 11 के अंतर्गत स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:
- “पूर्व वाद” शब्द का तात्पर्य ऐसे वाद से है जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद से पहले ही किया जा चुका है। चाहे ऐसा वाद विचाराधीन वाद से पहले ही शुरू किया गया हो, यानी वर्तमान वाद से पहले, “पूर्व वाद” शब्द को परिभाषित करते समय कोई फर्क नहीं पड़ता।
- किसी मामले में निर्णय देने की न्यायालय की क्षमता का निर्धारण, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से संबंधित प्रावधानों पर विचार किए बिना किया जाता है।
- वर्तमान वाद में जिस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, वह किसी पुराने वाद के संदर्भ में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वर्तमान वाद में मुद्दे पर एक पक्ष द्वारा दावा किया गया होगा और पूर्व वाद में दूसरे पक्ष द्वारा इसे अस्वीकार या स्वीकार किया गया होगा।
- पिछली कार्यवाही में उठाया गया कोई भी तर्क या बचाव सीधे और मूलतः ऐसे वाद का मुद्दा माना जाता है।
- यदि वादियों द्वारा वादपत्र में मांगी गई राहत न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की जाती है, तो इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह माना जाएगा कि मांगी गई ऐसी राहत को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।
- जहां कोई व्यक्ति सार्वजनिक अधिकार या निजी अधिकार के संबंध में सद्भावपूर्वक वाद दायर करता है, जिसे वह दूसरों के साथ साझा करता है, अन्य सभी व्यक्ति जिनका ऐसे अधिकारों में हित है या जो ऐसे अधिकारों को साझा करने वाले सभी अन्य लोगों को भी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के माध्यम से दावा करते हुए माना जाएगा, जिसने ऐसा वाद आरंभ किया है।
- यह धारा उन कार्यवाहियों पर लागू होती है, जहाँ न्यायालय अपने आदेश को लागू करता है। किसी भी वाद, मुद्दे या पूर्व वाद के संदर्भ को ऐसी प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) कार्यवाही, उनमें उठाए गए मुद्दों और किसी भी पिछली प्रवर्तन कार्यवाही के संदर्भ के रूप में समझा जाना चाहिए।
- एक ऐसा मुद्दा जिसकी सुनवाई, निर्णय और अंतिम रूप से निपटान सीमित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा किया गया हो, लेकिन जो ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम था, किसी भी बाद के वाद में पूर्व-न्याय के रूप में कार्य करता है। यह तब भी सत्य है जब वह न्यायालय नए वाद या बाद में उठाए गए ऐसे मुद्दे पर सुनवाई करने में सक्षम न हो।
पूर्व-न्याय का सिद्धांत
जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पूर्व-न्याय का सिद्धांत सीपीसी की धारा 11 द्वारा शासित है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो अदालतों को ऐसे मामले की जांच करने से रोकता है जिसकी सुनवाई, जांच और निपटारा पहले ही उसी न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। यह कानून के दुरुपयोग को रोककर न्याय के निष्पक्ष और ईमानदार प्रशासन को सुनिश्चित करता है। यह तब लागू होता है जब कोई पक्ष उसी विषय वस्तु के समान एक नया वाद शुरू करने का प्रयास करता है जिस पर न्यायालय द्वारा पहले ही उसी समूह के पक्षों से जुड़े किसी पिछले मामले में निर्णय लिया जा चुका है। पूर्व-न्याय का सिद्धांत न केवल उन दावों पर लागू होता है जो पहले के वाद में उठाए गए थे, बल्कि उन विशेष आरोपों पर भी लागू होता है जो विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में प्रारंभिक कार्यवाही के दौरान लगाए गए थे।
पूर्व-न्याय के लिए पूर्वापेक्षाएँ (प्रिरिक्विजिट)
पूर्व-न्याय लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) द्वारा न्यायिक निर्णय: निर्णय किसी ऐसे न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया होगा जो मामले में ऐसा निर्णय लेने के लिए सक्षम या अधिकृत हो।
- अंतिम और बाध्यकारी: निर्णय निर्णायक होना चाहिए और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होना चाहिए। इसके अलावा, इसे आगे अपील के अधीन नहीं होना चाहिए।
- गुण-दोष के आधार पर निर्णय: न्यायालय को मूल कानूनी मुद्दों पर विचार करना चाहिए तथा तदनुसार अपना निर्णय देना चाहिए।
- निष्पक्ष सुनवाई: दोनों पक्षों को अपना मामला प्रस्तुत करने और सुनवाई का निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए।
- पिछले निर्णय निर्णायक (कन्क्लूसिव) हैं: पिछला निर्णय सही था या गलत, यह प्रासंगिक (रेलेवेंट) नहीं है।
पूर्व-न्याय की प्रकृति और दायरा
पूर्व-न्याय कानून का एक सामान्य नियम है जो कानूनी प्रणाली के सभी कामकाज को नियंत्रित करता है। यह आम कानून के सिद्धांतों से प्राप्त दो सिद्धांतों पर आधारित है: पहला, सार्वजनिक नीति और आवश्यकता जो वादबाजी को समाप्त करना राज्य के हित में बनाती है; और दूसरा, यह सिद्धांत कि व्यक्तियों को एक ही कारण के लिए बार-बार कानूनी कार्यवाही के अधीन होने से कठिनाई का सामना नहीं करना चाहिए। इस प्रकार, यह सार्वजनिक नीति है जो पूर्व-न्याय के सिद्धांत की नींव के रूप में कार्य करती है।
सीपीसी की धारा 11 के अंतर्गत पूर्व-न्याय का दायरा निर्धारित किया गया है, जो कि प्रकृति में संपूर्ण नहीं है, लेकिन निरंतर विकसित होता रहता है। यह सिद्धांत मूल रूप से उच्च सार्वजनिक नीति के विचारों पर आधारित है। इसका उद्देश्य दो प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करना है:
- सबसे पहले, वादबाजी को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसका परिणाम अंतिम परिणाम होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी विवाद एक निश्चित समाधान पर पहुंचे।
- दूसरा, व्यक्तियों को एक ही तरह के वाद से दो बार परेशान नहीं होना चाहिए। उन्हें दोहरे खतरे से बचाया जाना चाहिए।
यह आकलन करते समय कि क्या बाद की कार्यवाही पूर्व-न्याय द्वारा प्रतिबंधित है, कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
- न्यायालयों की योग्यता,
- पक्ष और उनके प्रतिनिधि,
- मुद्देगत मामले और
- अंतिम निर्णय।
यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि एक ही पक्ष से जुड़े बाद के मुकदमों में जारी किए गए निर्णय मामले में पहले से तय मुद्दों के अनुरूप होने चाहिए। पूर्व-न्याय का सिद्धांत यह दावा करता है कि एक बार जब कोई मामला अंतिम रूप ले लेता है, तो उसे फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व-न्याय का सिद्धांत पक्षों को निर्णय के खिलाफ अपील करने के उनके अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकता है।
रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत
रचनात्मक पूर्व-न्याय के सिद्धांत को सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत विस्तृत किया गया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी मामले में जिसे पिछले वाद में बचाव के हिस्से के रूप में उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था, उसे उस वाद में सीधे और काफी हद तक सवालों के घेरे में माना जाएगा। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि न्यायालय में वास्तव में किए गए दावों और उन सवालों के बीच कोई अंतर नहीं है जो उठाए जा सकते थे लेकिन नहीं उठाए गए। रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत पक्षों को बाद की कार्यवाही में तर्क या बचाव उठाने से रोकता है जो उसी विषय वस्तु के संबंध में पहले उठाए जा सकते थे।
पूर्व-न्याय और रचनात्मक पूर्व-न्याय के बीच अंतर
निम्न तालिका पूर्व-न्याय और रचनात्मक पूर्व-न्याय के बीच अंतर के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करती है:
| पहलू | पूर्व-न्याय | रचनात्मक पूर्व-न्याय |
| दायरा | यह सीधे तौर पर उन मामलों पर लागू होता है जिन पर वास्तव में वाद चलाया गया था और निर्णय लिया गया था। | यह उन मामलों पर लागू होता है जिन पर वाद चलाया जा सकता था और निर्णय लिया जा सकता था। |
| आधार | मामले पर वास्तविक पूर्व निर्णय। | मामले पर संभावित निर्णय। |
| पिछले निर्णयों की आवश्यकता | इसके लिए गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय की आवश्यकता है। | इसका तात्पर्य यह है कि यह मामला पिछले वाद में उठाया जाना चाहिए था। |
| सम्मिलित किये गये मुद्दों के प्रकार | सीधे मुद्दे से संबंधित मामले। | ऐसे मामले जो मुद्दे में हो सकते थे और होने भी चाहिए थे। |
| न्यायालय की क्षमता | इसके लिए पिछली न्यायालय को अगले वाद पर निर्णय लेने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। | यह माना जाता है कि पिछली न्यायालय इस अप्रकाशित मुद्दे पर फैसला दे सकती थी। |
| रोकथाम | यह समान मुद्दों पर पुनः वाद चलाने से रोकता है। | यह उन नए मुद्दों पर वादबाजी को रोकता है जिन्हें पिछले वाद में उठाया जाना चाहिए था। |

प्रासंगिक मामले
मार्जिनसन बनाम ब्लैकबर्न बरो काउंसिल (1939)
साक्ष्य के नियम के रूप में विबंधन (एस्टॉपेल) पर रेम जुडिकेटम के सिद्धांत को मार्जिनसन बनाम बोरो काउंसिल (1939) के मामले में व्यक्त किया गया था। इसने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य का व्यापक नियम एक ही कारण के दावे को रोकता है। पूर्व-न्याय का सिद्धांत बताता है कि:
- इसमें अंतिम और निर्णायक न्यायिक निर्णय शामिल होता है, जिसका उद्देश्य समुदाय के सामान्य हितों की रक्षा के अर्थ में विवादों को सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में खारिज करना होता है।
- इसका उद्देश्य लोगों के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें बार-बार आने वाले मुद्दों या पहले से चल रहे मुकदमों से बचाना है।
हालांकि, इस बात पर भी जोर दिया गया कि पूर्व-न्याय का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक बल्कि निजी हितों की भी सेवा करना है, क्योंकि इससे पहले से ही निर्णय लिए जा चुके मामलों को फिर से खोलने में बाधा उत्पन्न होती है। यह एक ही कारण और एक ही हित के आधार पर एक ही सिविल दावे के लिए दूसरा निर्णय मांगने पर रोक लगाता है। बाद के मुकदमों में उन्हीं मुद्दों पर फिर से विचार करने से समान अधिकार क्षेत्र के निर्णयों में संघर्ष बढ़ सकता है। इससे बार-बार वाद हो सकते हैं और न्याय प्रशासन विवाद में आ सकता है। इस तरह की बार-बार की जाने वाली कार्रवाई न्यायिक निर्णयों की स्पष्टता और अधिकार को कमज़ोर करती है जब उन्हें सुनाया जाता है। वे अपनी पहचान और जीवंतता खो देते हैं।
ग्रीनहालघ बनाम मैलार्ड (1947)
ग्रीनहालघ बनाम मैलार्ड (1947) के मामले में, यह कहा गया था कि पूर्व-न्याय का उद्देश्य केवल उन मुद्दों तक सीमित नहीं था, जिन्हें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष तय किया जाना था। इसके बजाय, यह उन सभी तथ्यों और मुद्दों को कवर करता है जो वाद का हिस्सा हैं। पिछली कार्यवाहियों के आधार पर नई कार्यवाही दायर करने की अनुमति देकर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को दर्शाते हुए, विषय वस्तु के संबंध में मुद्दे उठाए गए थे।
देवीलाल मोदी बनाम बिक्री कर अधिकारी, रतलाम (1964)
देवी लाल मोदी बनाम बिक्री कर अधिकारी, रतलाम (1964) के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक ही पक्ष के बीच कई कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए सार्वजनिक नीति के विचारों पर, रचनात्मक पूर्व-न्याय का नियम लागू होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पक्ष ने अपने और विरोधियों के बीच पिछली कार्यवाही में कोई दलील दी है, तो वे उसी मुद्दे और कार्रवाई के समान कारण के आधार पर बाद की कार्यवाही में उसी पक्ष के खिलाफ वही दलील नहीं दे सकते। इस प्रकार, रचनात्मक पूर्व-न्याय का यह नियम पूर्ववर्ती रिट कार्यवाही पर लागू होता है।
गुलाबचंद छोटेलाल पारीख बनाम बॉम्बे राज्य (1964)
गुलाबचंद छोटेलाल पारीख बनाम बॉम्बे राज्य (1964) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व-न्याय के सिद्धांत और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 में उल्लिखित अवधि के दौरान इसकी प्रगति का उल्लेख किया। यह धारा, इसके स्पष्टीकरणों के साथ, सिद्धांत के लगभग पूरे उद्देश्य को सम्मिलित करती है। गुलाबचंद मामला पिछली कार्यवाही के समान था, लेकिन उच्च विशेषाधिकार रिट के मुद्दे पर इसका कोई सीधा अनुप्रयोग नहीं है। हालाँकि, बार-बार रिट आवेदनों से जुड़े मामलों में पूर्व-न्याय और रचनात्मक पूर्व-न्याय के सामान्य सिद्धांतों पर विचार किया गया है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पूर्व-न्याय का सिद्धांत तब भी लागू होता है जब प्रारंभिक कार्यवाही एक रिट वाद हो। न्यायालय ने कहा कि उन्होंने अभी तक इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या रचनात्मक पूर्व-न्याय को किसी पक्ष द्वारा बाद के वाद में लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुलाबचंद मामले की जांच में त्रुटि की है, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला कि रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत पिछली कार्यवाही में प्रासंगिक नहीं था। प्रतिवादी परिणामी वाद में अतिरिक्त दलील उठा सकता था, जो उसने पहले दायर की गई रिट याचिका में नहीं किया था।
संविधान के अनुच्छेद 226 का अवलोकन
संविधान का अनुच्छेद 226, भारतीय संविधान के भाग V के अंतर्गत निहित है। यह उच्च न्यायालयों को उचित मामलों में किसी भी सरकार को रिट जारी करने का अधिकार देता है। इन रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉरपस), परमादेश (मैंडेमस), निषेध (प्रोहिबिशन), अधिकार-पृच्छा (क्वो-वारंटो) और उत्प्रेषण (सर्टिओरारी) शामिल हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति देता है।
संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों को कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश और रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226(2) उच्च न्यायालयों की इस शक्ति को उन स्थितियों तक बढ़ाता है जहां कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है, जिससे उच्च न्यायालयों को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर सरकारी अधिकारियों या एजेंसियों को आदेश और रिट जारी करने की अनुमति मिलती है।
अनुच्छेद 226 का खंड (3) अंतरिम आदेशों से संबंधित है। जब किसी प्रतिवादी के खिलाफ उक्त अनुच्छेद के तहत निषेधाज्ञा या स्थगन की प्रकृति में अंतरिम आदेश जारी किया जाता है, तो प्रतिवादी ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। अनुच्छेद 226(3) के अनुसार, यदि प्रतिवादी आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन दायर करता है और आवेदन की एक प्रति उस पक्ष को देता है जिसके पक्ष में आदेश दिया गया था, तो उच्च न्यायालय को आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि के भीतर उसका निपटारा करना होगा। खंड यह भी निर्दिष्ट करता है कि यदि उच्च न्यायालय इस अवधि के भीतर कार्रवाई नहीं करता है, तो अंतरिम आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
अनुच्छेद 226 का खंड (4) स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालयों को दिया गया अधिकार क्षेत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से नहीं रोकता है।
यह स्थापित किया गया है कि, सामान्य अर्थ में, पूर्व-न्याय का नियम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के तहत कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान लागू नहीं होता है। एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत के रूप में पूर्व-न्याय का सामान्य नियम यह निर्धारित करता है कि रिट याचिकाएँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत खारिज किए जाने के अधीन हैं। हालाँकि, यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाएँ या अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर करने पर रोक नहीं लगाता है।
संविधान के अनुच्छेद 32 का अवलोकन
भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की मांग करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है, यदि उसका उल्लंघन हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश या रिट जारी करने की शक्ति और अधिकार है। रिट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा शामिल हैं। यह एक वैकल्पिक उपाय है जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत राहत पर कोई रोक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुसार इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या वित्तीय संकट जैसी आपात स्थिति की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के दौरान, एक पीड़ित पक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा सकता है। मूल क्षेत्राधिकार के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया में पक्ष को पहले अपील की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होती है।
समवर्ती (कंकररेंट) क्षेत्राधिकार के मामलों में, यदि किसी पीड़ित पक्ष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो उनके पास अनुच्छेद 226 के तहत निर्धारित अनुसार सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है।
मामले
एमाल्गमेटेड कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम जनपद सभा, छिंदवाड़ा (1961)
एमाल्गमेटेड कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम जनपद सभा, छिंदवाड़ा (1961) के मामले में वही पक्ष शामिल थे जो पिछले मामले में थे, जहां उन्हीं मुद्दों पर कोयला कर लगाए जाने को चुनौती देने के लिए रिट के रूप में याचिका दायर की गई थी। हालांकि याचिकाकर्ता ने इसे अतिरिक्त आधार के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी और याचिका खारिज कर दी गई। नतीजतन, अलग-अलग आधारों पर कर लगाने को चुनौती देने के लिए एक अलग वाद दायर किया गया, लेकिन न्यायालय ने इसे भी अस्वीकार कर दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि रिट को पूर्व-न्याय द्वारा प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि मामले पर न्यायालय का पिछला निर्णय पहले ही दर्ज किया जा चुका था। यही मुद्दा बार-बार दूसरे वाद में न्यायालय के समक्ष अपील के रूप में आया। निर्णय सुनाए जाने के दौरान, एक सीधा सवाल उठा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मुकदमों पर रचनात्मक पूर्व-न्याय के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कार्यवाही में नोटिस की वैधता को चुनौती, पहले उठाए गए आधारों से बिल्कुल अलग आधार पर दी गई थी। यह एक ही मुद्दे को एक बार फिर से न्यायालय के समक्ष लाने का मामला नहीं था, बल्कि अलग-अलग कार्यवाहियों में था। मुद्दे पूरी तरह से अलग थे। न्यायालय ने तब उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय के निर्णय को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट याचिकाओं पर रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत लागू हो। न्यायालय के विचार में, सीपीसी की धारा 11 में परिभाषित रचनात्मक पूर्व-न्याय, “पूर्व-न्याय का एक विशेष और कृत्रिम रूप है”। इसे आम तौर पर इन अनुच्छेदों के तहत दायर रिट याचिकाओं पर लागू नहीं किया जाता है।
दरियाओ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1961)
दरियाओ और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1961) के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-न्याय के नियम का विस्तार किया गया था। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के लिए शुरू में संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला दिया। हालाँकि, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला दिया और उन्हीं मुद्दों के लिए समान उपाय की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पिछला निर्णय अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के लिए पूर्व-न्याय के रूप में कार्य करता है। इसने याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को बरकरार रखा और याचिका को अस्वीकार कर दिया।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमाने तरीके से सेवा से निकाले जाने और बर्खास्त किये जाने से बचाता है। अनुच्छेद 311 की पृष्ठभूमि में कहा गया है कि:
- कोई भी व्यक्ति जो संघ या किसी राज्य की सिविल सेवा के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसे उस प्राधिकारी के अधीनस्थ (सब-ऑर्डिनेट) किसी प्राधिकारी द्वारा समाप्त या हटाया नहीं जाएगा, जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया था।
- किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जांच के बर्खास्त, समाप्त या पद से हटाया नहीं जाएगा, जिसमें उन्हें उनके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में बताया गया हो। अनुच्छेद 311 यह भी सुनिश्चित करता है कि उन्हें इन आरोपों के खिलाफ अपने बचाव में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए।
वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी ने सेवा समाप्ति आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उसे सुनवाई के लिए तथा आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया गया, जैसा कि अनुच्छेद 311 के अंतर्गत अपेक्षित है। मामले में प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डाला गया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 के अंतर्गत बताए गए अनुसार निष्पक्ष सुनवाई के बिना सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाए। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाले सभी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष दायर प्रारंभिक मामले में उठाया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन के मामले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 और पूर्व-न्याय के सिद्धांत के बीच परस्पर क्रिया को उजागर किया, जिसमें सिविल सेवकों के लिए कानूनी कार्यवाही की शुरुआत में अपनी शिकायतें उठाने के महत्व पर जोर दिया गया। इस मामले ने यह भी पुष्ट किया कि अनुच्छेद 311 के तहत निहित सुरक्षा और संरक्षण न्यायिक दक्षता (एफिशिएंसी) और अंतिमता को बनाए रखता है।
मामले का निर्णय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पक्षों के बीच उभरने वाला मुद्दा पूर्व-न्याय का गठन करता है, क्योंकि इसे रिट कार्यवाही में उठाया गया था। यह भी ध्यान दिया गया कि प्रतिवादी ने रिट याचिका में पुलिस उप महानिरीक्षक के उसे बर्खास्त करने के अधिकार को चुनौती नहीं दी। रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया गया था।
न्यायालय ने प्रश्न किया कि क्या रचनात्मक पूर्व-न्याय के सिद्धांत को उन मुद्दों पर लागू किया जा सकता है जो पिछली कार्यवाहियों में उठाए जा सकते थे या उठाए जाने चाहिए थे। न्यायालय ने कहा कि इस मामले के मुद्दे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुलाबचंद छोटेलाल पारीख बनाम बॉम्बे राज्य (1964) के मामले में खुला छोड़ दिया था, और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी की अपील को अनुमति दी गई थी।
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया, जैसे एल. जानकीराम अय्यर एवं अन्य बनाम पी.एम. नीलकंठ अय्यर एवं अन्य (1961), देवीलाल मोदी बनाम बिक्री कर अधिकारी, रतलाम एवं अन्य (1964), और गुलाबचंद छोटेलाल पारीख बनाम बॉम्बे राज्य, और निष्कर्ष निकाला कि पिछली याचिका में उठाया गया कोई भी मुद्दा पूर्व-न्याय माना जाएगा। वर्तमान मामले में, अनुच्छेद 226 के तहत दायर प्रारंभिक रिट याचिका में पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा समाप्ति आदेश की वैधता पर सवाल नहीं उठाया गया था। चूंकि यह मुद्दा पहले नहीं उठाया गया था, इसलिए इसे उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित नहीं किया गया था। वादी को बाद की कार्यवाही में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी गई थी। इस वाद में पूर्व-न्याय ने इसे रोका नहीं था।
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत मामले पर लागू होता है। इसने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवादी की नियुक्ति के बावजूद पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवादी की सेवा समाप्त करना वैध नहीं था। हालाँकि, न्यायालय ने न्यायिक नियम से संबंधित मुद्दों को हल करने में कानून की गलती की, जो न्यायालय के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं थे।
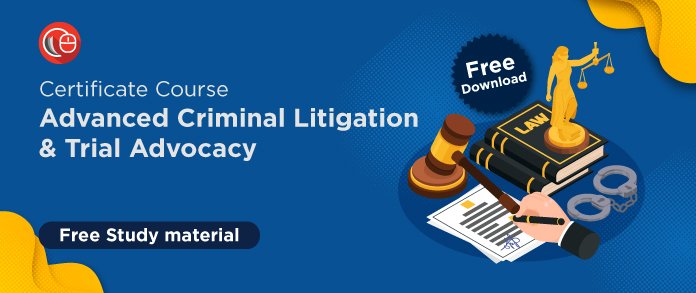
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मामला जिसे पिछली कार्यवाही में उठाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया गया, उसे कई मुकदमों को रोकने और अंतिमता सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक रूप से तय माना जाता है।
इस मामले में रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण प्रार्थना थी, जिसे प्रतिवादी के ज्ञान में लिया गया था और इसे रिट याचिका में उठाया जा सकता था, लेकिन नहीं उठाया गया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसे विभाग की जांच में उठाए गए आरोपों के खिलाफ सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, और इस प्रकार उसके खिलाफ की गई कार्रवाई कानून की नजर में अन्यायपूर्ण थी।
इसलिए, प्रतिवादी वर्तमान वाद में सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती नहीं दे सका। दूसरी ओर, बर्खास्तगी उसे नियुक्त करने वाले के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा की गई थी। इससे और भी कानूनी मुद्दे खड़े हो गए।
सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रचनात्मक पूर्व-न्याय के सिद्धांत पर विचार किए बिना पूर्व-न्याय मुद्दे पर अपना निर्णय सुनाते हुए गलती की थी। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में उठाए गए अन्य बिंदुओं की जांच करना अनावश्यक था।
न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने कहा कि रचनात्मक पूर्व-न्याय संहिता द्वारा स्थापित एक तकनीकी नियम है। इसका मतलब है कि अगर कोई पक्ष अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पिछले मामले में कोई तर्क दे सकता था, तो वे उसी मुद्दे पर आधारित और उन्हीं पक्षों को शामिल करने वाले बाद के मामले में उस तर्क को नहीं दे सकते। यह नियम रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी संविधान के अनुच्छेद 311(1) के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करने में विफल रहा। विशेष रूप से, प्रतिवादी ने यह तर्क नहीं दिया कि उसे पुलिस के डीआईजी द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, वह इस महत्वपूर्ण तर्क से पूरी तरह वाकिफ था लेकिन उसने इसे रिट याचिका में नहीं उठाया।
इसके बजाय, प्रतिवादी ने अन्य पहलुओं के बारे में तर्क दिया, जैसे कि विभागीय जांच में खुद का बचाव करने का अवसर। इसलिए, प्रतिवादी बाद के वाद में अलग-अलग आधारों पर अपनी बर्खास्तगी को चुनौती नहीं दे सकता था, जिन्हें पहले ही खारिज कर दिया गया था।
इस निर्णय के पीछे तर्क
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान संपूर्ण नहीं हैं। यह उन मामलों से संबंधित है जहां एक ही मामले पर एक ही पक्ष के बीच एक ही मामले पर एक ही पिछले निर्णय के बाद के सिविल मुकदमों में पूर्व-न्याय के रूप में कार्य करता है। सामान्य तौर पर, पूर्व-न्याय का सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी मामले पर पूरी तरह से बहस होने के बाद निर्णय सुनाया जाता है और पक्षों को सक्षम न्यायालय के समक्ष अपना मामला साबित करने का उचित अवसर दिया जाता है। यह सिद्धांत भविष्य के मुकदमों में उन्हीं मुद्दों और कार्रवाई के कारणों को फिर से वादबाजी से रोकता है। हालाँकि, यह अनिवार्य नहीं है कि भविष्य के मुकदमों या चल रही कार्यवाही में पूर्व-न्याय लागू होने के लिए न्यायालय को औपचारिक रूप से मामले का निर्णय करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन (1977) का विश्लेषण
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि रचनात्मक पूर्व-न्याय का सिद्धांत पहले से तय वाद पर रोक नहीं लगाता। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवादी को जारी सेवा समाप्ति का आदेश, जो पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कार्य कर रहा था, विवाद का विषय था। उच्च न्यायालय ने पूर्व-न्याय की प्रयोज्यता को खारिज करके तथा मामले में अन्य बिंदुओं की जांच को प्रतिबंधित करके कानूनी त्रुटि की।
मार्जिनसन बनाम ब्लैकबर्न बरो काउंसिल के मामले में, विबंधन पर रेम जुडिकेटम की अवधारणा, साक्ष्य का एक नियम, कार्रवाई के कारण के पुनः दावे को प्रतिबंधित करने के रूप में परिभाषित किया गया था। यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है:
- सार्वजनिक नीति के मामलों में विवादों के अंतिम निपटान के लिए अंतिम और निर्णायक निर्णय प्राप्त करना जो समुदाय के समग्र हित में काम करते हैं, और
- व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना ताकि उन्हें बार-बार वादबाजी से बचाया जा सके।
इसलिए, यह पहले से तय मामलों को फिर से खोलने से रोककर न केवल सार्वजनिक बल्कि निजी उद्देश्य भी पूरा करता है। यह एक ही मुद्दे और एक ही कारण से जुड़े सिविल वाद में दूसरा निर्णय प्राप्त करने पर रोक लगाता है। एक ही विषय वस्तु से जुड़ी बार-बार की जाने वाली कार्यवाही परस्पर विरोधी फैसलों और दोहराव वाली कार्रवाइयों को जन्म दे सकती है। यह बदले में भारतीय कानूनी प्रणाली की अखंडता को कमजोर कर सकता है।
तथ्यों का एक ही समूह कई कारणों को जन्म दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति को एक समय में एक कारण पर वाद करने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि अन्य मुद्दों को बाद के मुकदमों के लिए रोक दिया जाता है, तो इससे वादबाजी का बोझ बढ़ जाता है।
गुलाबचंद में स्थापित साक्ष्य के स्पष्ट और प्रभावी नियमों ने सीपीसी की धारा 11 के तहत कानूनी सिद्धांतों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। इस खंड में दिए गए स्पष्टीकरण क्षेत्र के लगभग सभी पहलुओं को कवर करते हैं और सिद्धांत के उद्देश्य को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं।
हालाँकि, ये नियम मुख्य रूप से पहले के मुकदमों और बाद के मुकदमों पर लागू होते हैं और रिट जारी करने के लिए याचिका पर इनका कोई सीधा अनुप्रयोग नहीं होता है। सामान्यतः, रिट के लिए नए सिरे से आवेदन के मामलों में पूर्व-न्याय और रचनात्मक पूर्व-न्याय के नियम लागू होते हैं।

निष्कर्ष
वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। शुरू में, उसने एक रिट याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई अन्यायपूर्ण थी। बाद में, उसने एक और याचिका दायर की जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसे पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था और इसलिए उसे उप महानिरीक्षक द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि डीआईजी को उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए, उनकी सेवा से बर्खास्तगी उस व्यक्ति द्वारा की गई जिसके पास उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था और इसलिए यह अवैध था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विभागीय जांच में आरोपों के खिलाफ उन्हें अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बाद की याचिका में उठाए गए तर्कों को प्रारंभिक रिट याचिका में शामिल किया जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रासंगिक था और पिछली रिट याचिका दायर करने के समय प्रतिवादी के ज्ञान में था। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए इस अपील को स्वीकार कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व-न्याय और रचनात्मक पूर्व-न्याय के सिद्धांतों के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
पूर्व-न्याय और न्यायाधीन मामला (रेस सब जुडिस) के सिद्धांत में क्या अंतर है?
पूर्व-न्याय और न्यायाधीन के सिद्धांत के बीच मुख्य अंतर अदालती कार्यवाही में उनके समय और स्थिति में निहित है। पूर्व-न्याय तब लागू होता है जब कोई मामला अपने अंतिम निर्णय पर पहुँच जाता है, जो उन्हीं पक्षों को उसी विषय पर फिर से वाद दायर करने से रोकता है। दूसरी ओर, रेस सब जुडिस तब लागू होता है जब कोई मामला अभी भी न्यायालय के समक्ष लंबित है, जो पक्षों को उसी मुद्दे पर समानांतर कार्यवाही शुरू करने से रोकता है।
विबंधन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
विबंधन का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करने से रोकता है जो उसके पिछले दावों या कार्यों के विपरीत हों।
पूर्व-न्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक बातें क्या हैं?
पूर्व-न्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक तत्वों को सर विलियम डी ग्रे, सी.जे. द्वारा डचेस ऑफ किंग्स्टन (1776) के मामले में रेखांकित किया गया है, और कहा गया है कि:
- न्यायालय के पास सक्षम क्षेत्राधिकार होना चाहिए।
- आगामी वाद में मुद्दा उन्हीं पक्षों के बीच होना चाहिए।
‘शायद’ (माईट) और ‘चाहिए’ (ऑट) के सिद्धांत में क्या अंतर है?
‘शायद’ और ‘चाहिए’ के सिद्धांत का विस्तार बहुत व्यापक है। ‘शायद’ का तात्पर्य बचाव के सभी आधारों को जोड़ने की संभावना के विचार से है। जबकि ‘चाहिए’ का तात्पर्य उन आधारों को जोड़ने के औचित्य या शुद्धता के विचार से है।
संदर्भ
- 18वां संस्करण, एम.पी.जैन, भारतीय संवैधानिक कानून
- 13वां संस्करण, वी.एन.शुक्ला, भारत का संविधान
- 9वां संस्करण, सी.के.तकवानी, सिविल प्रक्रिया संहिता