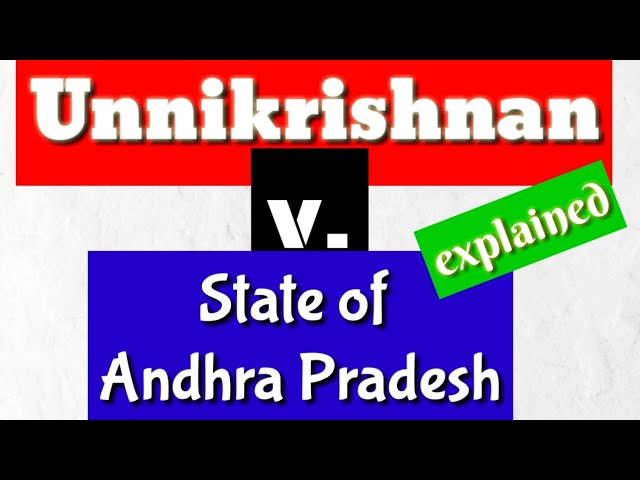यह लेख Arya Senapati द्वारा लिखा गया है। यह इस मामले में तथ्यों, कानूनी मुद्दों, तर्कों और निर्णय के बिंदुओं को निकालने के लिए उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के ऐतिहासिक फैसले का विश्लेषण करने का प्रयास करता है। इसे बेहतर समझने के लिए संवैधानिक कानून और अन्य कानूनी मामलों से संबंधित कानूनी सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
हर किसी ने ऐसी बातें सुनी हैं कि “उसका दाखिला प्रबंधन कोटे के तहत उस संस्थान में हुआ है” या “उसे दान के माध्यम से प्रवेश मिला है” और सोचा है कि नामांकन की ऐसी प्रक्रिया क्या होती है। प्रबंधन कोटा, दान सीटें और निजी सीटें कुछ और नहीं बल्कि एक प्रतिव्यक्ति शुल्क (कैपिटेशन फीस) है जो एक छात्र अपनी पसंद का पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए एक निजी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने के लिए भुगतान करता है। यह भुगतान आमतौर पर सरकारी संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले भुगतान से अधिक होता है।
विभिन्न मामलों में प्रतिव्यक्ति शुल्क की वैधता पर विचार किया गया है, क्योंकि यह भारत के सभी नागरिकों को उपलब्ध शिक्षा के अधिकार के विरुद्ध है। हालांकि, दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थानों ने हर बार यह तर्क दिया कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।
निजी शिक्षण संस्थानों को अपने संचालन के लिए निश्चित रूप से अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या ऐसी आवश्यकता के तहत प्रतिव्यक्ति शुल्क लगाने की अनुमति दी जा सकती है? यह प्रश्न भारत की अदालतों को वर्षों तक उलझन में डालता रहा और अंततः उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामले में निर्णय आया।

मामले का विवरण
- मामले का नाम: उन्नी कृष्णन, जे.पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।
- शामिल पक्ष: उन्नी कृष्णन, जे.पी. (याचिकाकर्ता) और आंध्र प्रदेश राज्य (प्रतिवादी)
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- पीठ:
- भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश एल.एम. शर्मा;
- माननीय न्यायमूर्ति एस.पी. भरूचा;
- माननीय न्यायमूर्ति एस.आर. पांडियन;
- माननीय न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी;
- माननीय न्यायमूर्ति जे.एस. मोहन।
- निर्णय की तिथि: 4 फरवरी, 1993
- उद्धरण: 1993 एआईआर 2178, 1993 एससीआर (1) 594, 1993 (1) एससीआर 594, (1993) 1 जेटी 474 (एससी)।
मामले की पृष्ठभूमि
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामले में चर्चा किए गए कानूनी प्रश्न पहली बार मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) के मामले में उठे थे। प्राथमिक प्रश्न भारत के नागरिक के चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक डिग्री-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के संबंध में इस प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं दिया कि यह अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार से संबंधित है या उसका हिस्सा है या नहीं, क्योंकि इस मामले में यह प्रश्न नहीं उठाया गया था।
वर्तमान मामले में, यह तर्क दिया गया कि चूंकि मोहिनी जैन मामले का निर्णय इस कानूनी प्रश्न पर सकारात्मक निष्कर्ष देता है कि क्या अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए गुण-दोष के आधार पर इस प्रश्न और इसकी शुद्धता पर विचार करना आवश्यक है, लेकिन उन्नीकृष्णन मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने इस तरह के विचार की आवश्यकता महसूस नहीं की।
मामले के तथ्य
तथ्यों का एक जटिल समूह अभी भी मौजूद है जिसके कारण यह मामला सामने आया। यह मामला शुरू में आंध्र प्रदेश राज्य से सामने आया और फिर भारत के कई अन्य राज्यों के खिलाफ भी कई याचिकाएं दायर की गईं। इस मामले में चार राज्य शामिल थे।
25 मई, 1992 को आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य भर में मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन आमंत्रित किये। ऐसे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 जून, 1992 निर्धारित की गई। जो लोग मेडिकल महाविद्यालयो के लिए आवेदन कर रहे थे, उनसे एक करोड़ रुपये जमा कराने, एक करोड़ रुपये की बैंक गारंटी तथा चार करोड़ रुपये की वित्तीय क्षमता के पर्याप्त सबूत देने को कहा गया था।
आवेदकों द्वारा प्रस्तावित भूमि एवं अन्य दायित्वों के निरीक्षण हेतु एक समिति गठित की गई। इसके बाद समिति ने दिशा-निर्देश तैयार किये और रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 12 मेडिकल महाविद्यालयो और 8 डेंटल महाविद्यालयो की सिफारिश की गई। मुख्यमंत्री ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी और ऐसा करने की अनुमति देते हुए एक सरकारी आदेश प्रकाशित किया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं।
चुनौती का आधार यह था कि राज्य में विभिन्न निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हो रहे थे और शैक्षणिक वर्ष 1992-93 तक इन निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयो में सीटें योग्यता के आधार पर एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाती थीं। इन संस्थानों के प्रबंधन के पास प्रवेश के मामले पर कोई नियंत्रण या विकल्प नहीं था। उन्हें प्रवेश के लिए सरकारी संस्थान से अधिक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी।
जैसे ही 15 अप्रैल, 1992 को तेलंगाना शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश विनियमन और प्रतिव्यक्ति शुल्क निषेध) अधिनियम, 1983 की धारा 3A लागू की गई, निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयो ने मांग की कि उन्हें योग्यता की परवाह किए बिना, अपनी पसंद के आधार पर आधी सीटों तक छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है। प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर दिया जाएगा।
इस हंगामे का मूलतः यह मतलब था कि वे बिना किसी विनियमन के अपनी इच्छानुसार भारी प्रतिव्यक्ति शुल्क लगाने का अधिकार चाहते थे। इससे छात्रों और शिक्षकों में अशांति पैदा हो गई, जिन्होंने इस तरह के प्रवेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
सरकार अशांति की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं कर सकी और उसने निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयो पर दबाव डाला कि वे तब तक कोई प्रवेश न दें जब तक कि धारा 3A के अनुसार स्पष्ट नियम नहीं बना लिए जाते। इंजीनियरिंग महाविद्यालयो ने इस आधार पर आदेश का विरोध किया कि उन्होंने पहले ही अपनी पसंद के आधार पर 50% सीटों पर प्रवेश दे दिया है।
इन विशेष प्रवेश के कारण आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने उक्त रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया तथा धारा 3A को संवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयो द्वारा अपनी पसंद के आधार पर आधी सीटों पर दिए गए प्रवेश पूरी तरह से अवैध हैं।
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 12 मेडिकल महाविद्यालयो और 8 डेंटल महाविद्यालयो को अनुमति देने वाला सरकारी आदेश मूलतः अवैध है। इस निर्णय और आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन द्वारा प्रवेश दिए गए छात्रों ने इस निर्णय का विरोध किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं गई।
भारत के कई अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की याचिकाएं दायर की गईं।
वर्तमान मामले में अन्य राज्यों की संलिप्तता (इन्वॉल्वमेंट)
चूंकि मामले में शामिल मुद्दे राष्ट्रीय थे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि देश के सभी राज्यों को वर्तमान मामले में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन केवल आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक ही इस मामले में उपस्थित हुए थे। उन्नीकृष्णन मामले में उपस्थित सभी मामले मुख्यतः इन चार राज्यों से संबंधित थे।

शामिल कानूनी मुद्दे
वर्तमान मामले में शिक्षा के अधिकार से संबंधित विभिन्न कानूनी मुद्दे शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन प्राथमिक कानूनी मुद्दों पर निर्णय दिया वे निम्नलिखित थे:
- क्या मोहिनी जैन के मामले में दिया गया निर्णय उसकी योग्यता के आधार पर सही है?
- क्या शिक्षा का अधिकार एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार है जिसे भारत के नागरिक संविधान के आधार पर प्राप्त करने के हकदार हैं?
- क्या नागरिकों को दी गई शिक्षा के अधिकार की गारंटी के तहत प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने का विचार उचित है?
- क्या शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतिव्यक्ति शुल्क लगाना मनमाना, अनुचित, अन्यायपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?
पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ताओं (निजी शिक्षण संस्थानों) ने निम्नलिखित बिंदुओं पर तर्क दिया:
- शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(g) के आधार पर प्रत्येक नागरिक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का मौलिक अधिकार है और ऐसा अधिकार उन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को भी शामिल करता है जिनका उद्देश्य व्यवसाय से पहले लाभ कमाना है। अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह इस अधिकार पर भी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन वैध प्रतिबंधों को छोड़कर यह अधिकार पूर्ण अधिकार है।
- वास्तविक समस्या निजी प्रकृति की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना में नहीं, बल्कि अनावश्यक रूप से राज्य के नियंत्रण में है। ऐसे संस्थानों की मांग उन लोगों द्वारा की जाती है जो वहां अध्ययन करने में सक्षम हैं तथा अपनी इच्छित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं, इसलिए मांग और आपूर्ति का मुक्त प्रवाह बनाए रखा जाना चाहिए।
- एक शैक्षणिक संस्थान का उद्यम, जो कि निजी प्रकृति का है, अन्य व्यावसायिक उद्यमों से बहुत भिन्न नहीं है और यह अप्रासंगिक है कि इन संस्थानों का उद्देश्य लाभ कमाना है या नहीं। जहां भी लाभ की भावना होगी, वहां पर्याप्त साधन वाले व्यक्ति अधिक विद्यालय और महाविद्यालय खोलेंगे तथा सभी वर्गों के लिए शिक्षा सुलभ कराएंगे। वर्तमान समय में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो परोपकारी ढंग से शैक्षणिक संस्थाओं का रखरखाव और प्रबंधन करते हैं।
- यदि सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य को बरकरार रखता है कि किसी व्यक्ति को व्यवसायिक उद्यम के रूप में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है, तो कम से कम उस व्यक्ति को स्व-वित्तपोषित (सेल्फ फाइनेंस्ड) शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार होना चाहिए। ऐसे संस्थानों को लागत-आधारित शैक्षणिक संस्थान कहा जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये संस्थान उन व्यक्तियों से अपनी इच्छानुसार शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगे जो शुल्क का भुगतान करने में सक्षम हैं, ताकि वे अपने बच्चों को वांछित पाठ्यक्रमों में दाखिला दिला सकें। ऐसी राशि से न केवल शैक्षणिक संस्थान चलाने के सामान्य व्यय (एक्सपेंडिचर) को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि विविधीकरण (डायवर्सिफिकेशन), विस्तार और विकास लागत को भी पूरा किया जा सकेगा। सरकार को ऐसे संस्थानों में शुल्क निर्धारण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकताएं शिक्षा के स्तर और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। सरकार निश्चित रूप से यह शर्त लगा सकती है कि ऐसे स्व-वित्तपोषित संस्थानों में कुछ सीटें उन मेधावी (मेरिटोरियस) छात्रों के लिए आरक्षित करेगी, जो सरकारी संस्थानों के समान ही शुल्क का भुगतान करेंगे। यह शर्त क्षमतावान और मेधावी दोनों प्रकार के छात्रों को सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देती है।
- मोहिनी जैन मामले में दिया गया निर्णय सही नहीं था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की सीमा से अधिक राशि वसूलना प्रतिव्यक्ति शुल्क है। इस प्रस्ताव से निजी शिक्षण संस्थानों के लिए अपना परिचालन जारी रखना तथा अपने खर्चों को पूरा करना असंभव हो जाएगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की लागत निस्संदेह अधिक है और राज्य संस्थानों में ऐसी लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है, लेकिन सरकार निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कोई अनुवृत्ति (सब्सिडी) नहीं देती है।
- भले ही अदालतें इस प्रस्ताव को बरकरार रखती हैं कि शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 19(1)(g) के अर्थ में व्यापार या कारोबार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, फिर भी यह निस्संदेह अनुच्छेद में मौजूद शब्द के अर्थ में एक व्यवसाय है। यह चार शब्द अर्थात पेशा, व्यवसाय, व्यापार और कारोबार का उल्लेख अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के व्यापक विस्तार को शामिल करने के लिए किया गया है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह बताना महत्वपूर्ण नहीं है कि उनकी गतिविधि किस अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है।
- शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार भी अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। संविधान निर्माताओं का आशय बहुसंख्यक समुदायों को वंचित करके केवल अल्पसंख्यकों के अधिकार को सीमित करने का नहीं हो सकता था और इसलिए, ऐसी व्याख्या को भी बरकरार रखा जा सकता है।
- निजी शिक्षण संस्थाओं को केवल मान्यता देने या संबद्ध करने से वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य के साधन या एजेंसी नहीं बन जाते हैं और इसलिए राज्य की कार्रवाई या कार्य की विशेषताओं को ऐसे महाविद्यालयो पर लागू नहीं किया जा सकता है, जिससे उन्हें संविधान के भाग III के अनुशासनात्मक दायरे में लाया जा सके। यदि संस्थान को राज्य से कोई सहायता प्राप्त हो रही हो तो मामला अलग हो जाता है। ऐसी स्थितियों में, अनुच्छेद 29(2) का प्राधिकार सामने आता है, लेकिन तब भी यह संस्थानों को केवल योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं करता है, बल्कि उन्हें केवल उल्लेखित आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से इनकार करने की अनुमति देता है।
प्रतिवादी
प्रतिवादियों (भारत के विभिन्न राज्यों) ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर तर्क दिया:
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि भारत में हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्म शिक्षा को धार्मिक कर्तव्य मानते हैं तथा इसे कभी भी व्यवसाय या व्यापार नहीं माना गया है। इसे एक उद्देश्य के रूप में माना गया है, न कि एक व्यापार के रूप में माना गया है। शिक्षा का व्यावसायीकरण राष्ट्र की संस्कृति के विरुद्ध है तथा राष्ट्र की नीतियों के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के कानून बनाने के पीछे संसद की मंशा स्पष्ट थी, क्योंकि इसका उद्देश्य शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना था।
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि शिक्षा प्रदान करना राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और यह कार्य राज्य द्वारा सीधे या निजी शिक्षण संस्थानों जैसे राज्य के माध्यम से किया जा सकता है। जब भी राज्य किसी निजी संगठन या व्यक्ति को राज्य के कार्य करने की अनुमति देता है, तो यह राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी को आर्थिक श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश या प्राथमिकता न मिले, जिससे अन्य छात्रों की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- शिक्षा की लागत वसूलने का विचार ही लागत आधारित या स्व-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों को कार्य करने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसा कार्य नैतिक रूप से गलत है और जनता के हितों के विपरीत है। प्रतिव्यक्ति शुल्क को केवल इसलिए गैर-प्रतिव्यक्ति शुल्क नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह लागत-आधारित या स्व-वित्तपोषित संस्थान चलाने के नाम पर लिया जाता है। प्रतिव्यक्ति शुल्क को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी शब्दावली, प्रवेश के लिए प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला महज दिखावा है। इससे समाज के एक वर्ग का शोषण होता है और यह काफी हद तक अभिजात्यवादी प्रकृति का है, जो संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इससे वर्गीय पूर्वाग्रह पैदा होता है और निम्न वर्ग के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।
- यदि किसी भी कारण से सर्वोच्च न्यायालय यह मानता है कि किसी नागरिक या व्यक्ति को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, तो यह अधिकार सरकार से संबद्धता या मान्यता प्राप्त करने के अतिरिक्त अधिकार को जन्म नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी कहा है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को भी संबद्धता या मान्यता का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए ऐसा अधिकार बहुसंख्यक समुदाय या व्यक्तियों को भी नहीं दिया जा सकता है। यदि किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के ऐसे अधिकार को मान्यता दी जाती है, तो राज्य या विश्वविद्यालयों को मान्यता या संबद्धता प्रदान करने तथा योग्यता, निष्पक्षता, शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और अन्य हितों को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्तें लागू करने का अधिकार होगा। सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं पर यह शर्त लागू कर दे कि वे केवल योग्यता के आधार पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश दें सकते है। राज्य सरकार के पास ऐसे शैक्षणिक संस्थानों से मान्यता या संबद्धता वापस लेने का विकल्प भी होगा, यदि सरकार द्वारा उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन या विचलन होता है।
- यदि किसी भी परिस्थिति में सरकार निजी शिक्षण संस्थानों पर ऐसी शर्तें नहीं लगाती है, तो ऐसी शर्तें लगाई जाएंगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में निजी शिक्षण संस्थान राज्य कार्रवाई करने वाले राज्य के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। यह तथ्य कि शिक्षा एक प्राथमिक सार्वजनिक कार्य है और राज्य प्रक्रियाओं के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है, उनके संचालन को एक राज्य कार्रवाई बनाता है। कम से कम, उनसे विद्यार्थियों के प्रवेश तथा शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में निष्पक्ष आचरण करने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों को कोई भी शुल्क नहीं लेना होगा जो समान पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सरकारी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली शुल्क से अधिक हो। अतिरिक्त वित्तीय एवं व्यय की स्थिति में, इन संस्थाओं को दान या धार्मिक एवं धर्मार्थ संगठनों से सहायता प्राप्त कर अपनी पूर्ति करनी पड़ती है। इन संस्थाओं को यह मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे पहले प्रतिव्यक्ति शुल्क जमा करें और फिर संस्था स्थापित करें। छात्रों से केवल न्यूनतम परिचालन लागत ही ली जा सकती है, भारी पूंजीगत लागत नहीं ली जा सकती है।

फैसले का तर्क
वर्तमान मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं को बरकरार रखा:
- भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है। इसकी सीमा अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 41 के संबंध में निर्धारित की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो, प्रत्येक नागरिक को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और इसलिए शिक्षा का अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता की व्यक्तिपरक सीमाओं पर निर्भर करता है।
- अनुच्छेद 41, 45 और 46 द्वारा सृजित दायित्वों का निर्वहन राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा निजी शैक्षणिक संस्थानों को सहायता, मान्यता और सम्बद्धता प्रदान करके किया जा सकता है। गैर-सहायता प्राप्त संस्थान अधिक शुल्क ले सकते हैं।
- प्रत्येक नागरिक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन संबद्धता, मान्यता या सहायता पाने का अधिकार नहीं है। संबद्धता या मान्यता के बिना, संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्री या प्रमाण पत्र का कोई मूल्य नहीं होता है और इसलिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार निरर्थक है।
- आंध्र प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश विनियमन एवं प्रतिव्यक्ति शुल्क प्रतिषेध) अधिनियम, 1983 की धारा 3A को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया, इसलिए यह असंवैधानिक एवं शून्य है।
- मोहिनी जैन के निर्णय को उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के मामले में दिए गए निर्णय के माध्यम से उलट दिया गया। निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिक शुल्क की वसूली जा सकती है। उच्चतर शुल्क सीमा सरकारी समिति द्वारा तय की जानी चाहिए तथा इससे अधिक लिया जाने वाला कोई भी शुल्क प्रतिव्यक्ति शुल्क समझा जाएगा। इस प्रकार की प्रतिव्यक्ति शुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक एवं अनुपूरक हैं। यद्यपि डीपीएसपी लागू करने योग्य नहीं हैं और मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, फिर भी दोनों के बीच यही एकमात्र अंतर है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में सहायता करेंगे और इसके विपरीत भी सहायता करेंगे।
द्विअर्थी (ऑबिटर डिक्टा) और निर्णय के पीछे का तर्क
इस निर्णय में कहा गया कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने का आशय रखने वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिकाएं मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) के मामले में विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की सत्यता को चुनौती देती हैं।
यहां याचिकाकर्ता वे लोग थे जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में मेडिकल या इंजीनियरिंग महाविद्यालय चलाते थे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि मोहिनी जैन मामले में लिए गए निर्णय को सही माना गया और फिर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया गया तो संस्थानों को अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि मोहिनी जैन मामले में फैसला वास्तव में क्या कहता है।
मुद्दा 1: मोहिनी जैन मामले की सत्यता
कर्नाटक सरकार की राज्य विधायिका ने कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति शुल्क का निषेध) अधिनियम, 1984 पारित किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के व्यावसायीकरण की बुरी और दुर्भावनापूर्ण प्रथा पर अंकुश लगाना था, क्योंकि इससे राज्य में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने में मदद नहीं मिली है और इसलिए इस व्यापक प्रथा पर अंकुश लगाना आवश्यक समझा गया।
प्रतिव्यक्ति शुल्क को किसी भी ऐसी राशि के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी शैक्षणिक संस्थान के निर्धारित शुल्क से अधिक भुगतान की गई हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वसूली गई हो। अधिनियम की धारा 3 किसी भी शैक्षणिक संस्थान या ऐसे संस्थान के प्रबंधन से संबंधित किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूलने पर रोक लगाती है।
अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से शिक्षण शुल्क या किसी अन्य शुल्क और जमा राशि को विनियमित करने के लिए सक्षम है, जिसे कोई शैक्षणिक संस्थान छात्रों की किसी भी या सभी कक्षाओं के लिए एकत्र या प्राप्त कर सकता है।
धारा 4 में कहा गया है कि किसी निजी शिक्षण संस्थान में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या तथा प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं सरकार द्वारा तय की जाएंगी।
अधिनियम की धारा 5 के तहत कर्नाटक सरकार को प्रदत्त शक्ति के आधार पर, सरकार ने 5 जून 1989 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि 1989-90 के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से, निजी मेडिकल महाविद्यालयो में देय शुल्क सरकारी सीटों पर भर्ती छात्रों के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष, कर्नाटक के छात्रों के लिए 25,000 रुपये और गैर-कर्नाटक छात्रों के लिए 60,000 रुपये होगा।
मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली गैर-कर्नाटक छात्रा मोहिनी जैन ने कर्नाटक के एक निजी मेडिकल महाविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया। महाविद्यालय ने उसे बताया कि उसे पहले वर्ष की ट्यूशन शुल्क के लिए 60,000 रुपये का भुगतान करना होगा तथा पाठ्यक्रम के शेष वर्षों के लिए देय शुल्क के लिए बैंक गारंटी देनी होगी।
यह देखते हुए कि उसके माता-पिता मांगी गई राशि का भुगतान करने की वित्तीय स्थिति में नहीं थे, उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। मोहिनी जैन ने बताया कि उनसे संस्थान में प्रवेश लेने के लिए 4,50,000 रुपये प्रतिव्यक्ति शुल्क मांगी गई थी, लेकिन शैक्षणिक संस्थान ने ऐसी किसी भी मांग से इनकार किया।
मोहिनी ने अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी, जिसमें कर्नाटक और गैर-कर्नाटक छात्रों के लिए अलग-अलग शुल्क की आवश्यकता थी। उन्होंने सरकारी सीटों पर दाखिला लेने वाले कर्नाटक के छात्रों द्वारा देय समान शुल्क का भुगतान करके दाखिला लेने की अनुमति मांगी।
अदालत ने कानूनी मुद्दों पर विचार किया और माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 38, 39 (a), 41 और 45 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर, संविधान के प्रारूपकारों का इरादा था कि राज्य के लिए सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य हो। यह देखा गया कि संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, वे राज्य के सभी नागरिकों को शिक्षा प्रदान किए बिना पूरे नहीं हो सकते तथा शिक्षा के प्रावधान के बिना किसी व्यक्ति की गरिमा को उचित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
यह कहा गया कि भारतीय संविधान के भाग III और भाग IV एक दूसरे के पूरक हैं तथा अनुच्छेद 41 के अनुसार शिक्षा के अधिकार को वास्तविकता में बदला जाना चाहिए ताकि भाग III में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को पूर्ण प्रभाव प्रदान किया जा सके। शिक्षा के बिना नागरिकों द्वारा मौलिक अधिकारों का समुचित रूप से क्रियान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) या उपयोग नहीं किया जा सकता है।
प्रतिव्यक्ति शुल्क के आधार पर न्यायालय ने कहा कि यह कुछ और नहीं बल्कि प्रवेश प्राप्त करने तथा शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए मात्र एक उपाय है। भारतीय संविधान में शिक्षा के व्यावसायीकरण की अवधारणा की परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए भारत में शिक्षा को बिक्री के लिए वस्तु नहीं बनाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा राज्य को सभी नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थान बनाने का दायित्व सौंपा गया है। राज्य को राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से इस दायित्व को पूरा करने की अनुमति है।
अदालत ने यह भी माना कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिव्यक्ति शुल्क को लागू करने की अनुमति देने की राज्य की कार्रवाई एक मनमाना कार्य था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। प्रतिव्यक्ति शुल्क लगाने से विभिन्न आर्थिक समूहों के लोगों के बीच गंभीर असमानता और पूर्वाग्रह पैदा होता है।
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि प्रवेश के लिए 60,000 रुपये लेना प्रतिव्यक्ति शुल्क लगाने के बराबर है। यह गैर-कर्नाटक छात्रों से भारी रकम वसूलने के लिए ली जाने वाली प्रतिव्यक्ति शुल्क का एक रूप है।
सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि यदि सरकार ने सरकारी महाविद्यालयो और सरकारी सीटों वाले निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष ट्यूशन शुल्क तय की है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए भी पर्याप्त कदम उठाने चाहिए कि कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अन्य छात्रों से प्रवेश के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक शुल्क न ले।
कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी कोई राज्य सरकार किसी निजी शैक्षणिक संस्थान को महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति देती है और किसी विशेष पाठ्यक्रम को चलाने के लिए उसके पाठ्यक्रम को मंजूरी देती है, तो निजी संस्थान संविधान के तहत राज्य को दिए गए कार्यों को पूरा कर रहा होता है। इस तर्क के आधार पर, कर्नाटक राज्य से बाहर के छात्रों पर प्रति वर्ष 60,000 रुपये का जुर्माना लगाना यह कुछ और नहीं बल्कि एक प्रतिव्यक्ति शुल्क है, जिसे कानून के तहत बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे हटाया जाना चाहिए।
रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मोहिनी जैन को प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रवेश नहीं मिला था और पाठ्यक्रम मार्च-अप्रैल 1991 में ही शुरू हो चुका था, लेकिन निर्णय 1992 में दिया गया।
उन्नीकृष्णन मामले पर विचार कर रही पीठ ने कहा कि उसका सरोकार पिछले मामले में उठे विशिष्ट प्रश्नों से नहीं है, बल्कि उसका सरोकार केवल मोहिनी जैन के फैसले की सत्यता से है, जिसे तीन प्राथमिक प्रश्नों में विभाजित किया जा सकता है, जो वर्तमान मामले उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) के लिए कानूनी मुद्दे हैं। पहला यह कि क्या भारत के संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या किसी भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 19(1)(g) या भारतीय संविधान के किसी अन्य प्रावधान के तहत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक अधिकार है। अंतिम प्रश्न यह था कि क्या विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन की अनुमति प्रदान करने से शैक्षणिक संस्थानों पर यह दायित्व आ जाता है कि वे विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश के मामले में बिना किसी पूर्वाग्रह या मनमानी के काम करें।
मुद्दा 2: भारतीय संविधान के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार
इस कानूनी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मानने और लागू करने के लिए संविधान में उसका स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक नहीं है।
एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम भारत संघ (1959) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न एक मौलिक अधिकार है।
इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 21 से अधिकारों का एक अलग समूह तैयार किया गया है, जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता और शीघ्र सुनवाई का अधिकार, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सम्मान और निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 21 उन अन्य अधिकारों के लिए एक छत्र है, जिनका मूल अधिकारों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि जैसे अधिकार शामिल हैं।
यद्यपि इस अनुच्छेद को नकारात्मक ढंग से लिखा गया है, लेकिन इसका उद्देश्य एक व्यापक व्याख्या करना था, जिसमें विभिन्न प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सच्ची प्राप्ति का गठन करते हैं। जबकि अनुच्छेद 19(1) मानव जीवन के लिए आवश्यक अधिकारों के एक विशेष समूह से संबंधित है, अवशिष्ट अधिकार जो अनुच्छेद 19 में उल्लिखित नहीं हैं, अनुच्छेद 21 में “व्यक्तिगत स्वतंत्रता” की व्यापक व्याख्या द्वारा शामिल किए गए हैं। यह व्याख्या कानून में काफी लम्बे समय से कायम है।
इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) के फैसले का हवाला दिया और कहा कि संवैधानिक सिद्धांतों की योजना में अनुच्छेद 21 के उद्देश्यों को सही मायने में पूरा करने के लिए “जीवन” शब्द की व्याख्या विस्तृत और व्यापक होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के उस हिस्से का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार के अंतर्गत कई पहलू शामिल हैं। यह जीवन के भौतिक अस्तित्व को नहीं समझता, जिसे मृत्युदंड या कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से छीना जा सकता है।
जीवन का भौतिक और शाब्दिक अर्थ, जीवन के अधिकार का मात्र एक पहलू है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले अन्य अधिकार, जैसे आजीविका का अधिकार भी मौलिक अधिकार का समान रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कोई भी चीज जो जीवन और जीवनयापन को टिकाऊ बनाती है तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसे अभिन्न रूप से जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाना चाहिए। जब राज्य अपने नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है, तो उसी अधिकार को मौलिक अधिकारों, विशेषकर जीवन के अधिकार के दायरे से बाहर रखना अनुचित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984) मामले का संदर्भ देते हुए यह स्पष्ट किया कि किस प्रकार पूर्व उदाहरण दर्शाते हैं कि मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 21 की व्याख्या डी.पी.एस.पी. के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के उस हिस्से को दोहराया जिसमें कहा गया है कि मानव सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है और इसका सार डीपीएसपी, विशेषकर अनुच्छेद 39 और 41 से प्राप्त होता है।

इन निर्णयों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि न्यायपालिका लगातार इस सिद्धांत को कायम रखती रही है कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के अनुपूरक एवं पूरक हैं। अदालतें इस बात पर भी जोर देती रही हैं कि संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों की व्याख्या प्रस्तावना और राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में की जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि यद्यपि न्यायपालिका ने शुरू में संविधान के भाग IV, अर्थात् राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के महत्व पर विशेष जोर देने में झिझक दिखाई थी, लेकिन अब यह झिझक समाप्त हो गई है।
यद्यपि मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोराईराजन (1951) के मामले में यह माना गया था कि राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों की तुलना में मौलिक अधिकार प्रमुख स्थान रखते हैं, लेकिन तब से इस समझ में बड़ा बदलाव आया है और इस मामले में न्यायालयों की धारणा में बदलाव आया है, जो मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच परस्पर क्रिया की अनुमति देता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने हनीफ बनाम बिहार राज्य (1959) मामले में लिए गए दृष्टिकोण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बल्कि अदालतों को इन दोनों सिद्धांतों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनीयस) व्याख्या प्रदान करनी चाहिए।
इन सभी मामलों और सिद्धांतों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय संविधान के भाग III और IV दोनों एक दूसरे के अनुपूरक और पूरक हैं तथा मौलिक अधिकार संविधान के भाग IV में दर्शाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन हैं। यह भी माना गया कि मौलिक अधिकारों को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से समझा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि वह पहले कानूनी मुद्दे पर इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहती है।
अनुच्छेद 21 और शिक्षा का अधिकार
बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार के अंतर्गत शैक्षणिक सुविधाएं भी शामिल हैं। व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन में शिक्षा के परम महत्व को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामले में दिए गए निर्णय के तर्क से सहमति व्यक्त की कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के अधिकार से उत्पन्न होता है। शिक्षा का अधिकार व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे भारत तथा विश्व में दशकों से मान्यता प्राप्त है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मोहिनी जैन मामले के निर्णय में शिक्षा के महत्व पर उचित एवं न्यायसंगत रूप से बल दिया गया था। न्यायालय ने मोहिनी जैन मामले में की गई इस टिप्पणी से सहमति व्यक्त की कि शिक्षा के बिना संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना असंभव है। अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि शिक्षा के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग IV में तीन बार तथा भाग III में दो बार किया गया है। यह तथ्य अपने आप में भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब राज्य कानून के बल पर किसी व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है, तभी अनुच्छेद 21 पर चर्चा की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह विशेष तर्क केवल वास्तविक मुद्दे के संबंध में भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया था। पहला कानूनी मुद्दा यह था कि क्या अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, और उसके बाद ही राज्य द्वारा इस अधिकार को छीनने का प्रश्न सामने आया।
केवल इस तथ्य से कि राज्य किसी व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर रहा है, यह तात्पर्य नहीं निकलता कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार से बाहर रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी अधिकार की व्याख्या उसके प्रति खतरे की धारणा पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए जीवन के अधिकार के घटक किसी ऐसी परिस्थिति के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करते जो इसके वंचन का कारण बन सकती हो। जीवन के अधिकार के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शिक्षा के अधिकार को कायम रखने का मूल तत्व यह है कि राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मोहिनी जैन मामले में लिया गया निर्णय इस तथ्य के संबंध में सही था कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से उत्पन्न होता है। अदालत के अनुसार, वास्तविक प्रश्न यह था कि अधिकार की वास्तविक सीमा क्या है और राज्य को प्रत्येक व्यक्ति को किस स्तर की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।
सरल शब्दों में कहें तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वास्तविक मुद्दा यह है कि नागरिक राज्य से मांग करते हैं कि वह उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराए। उक्त मुद्दे के संबंध में, मोहिनी जैन मामले के निर्णय में कहा गया है कि नागरिक ऐसी मांग कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में न्यायालय ऐसी व्यापक व्याख्या को बरकरार रखने से इनकार करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उत्पन्न होता है, की व्याख्या संविधान के भाग IV के प्रकाश में की जानी चाहिए, जिसके कई प्रावधान शिक्षा के अधिकार से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था और बीमारी की स्थिति में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करने के लिए बाध्य है।
अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा।
अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार है।
ये तीनों लेख विशेष रूप से सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य से संबंधित हैं। अनुच्छेद 45 और 41 के संदर्भ में, शिक्षा के अधिकार का अर्थ है कि भारत के प्रत्येक बच्चे या नागरिक को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होगी तथा बच्चे या नागरिक द्वारा 14 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, उसका शिक्षा का अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता की सीमाओं के भीतर कार्य करेगा।
इन कारकों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह सरल प्रश्न पूछा है कि संविधान लागू होने के इतने लम्बे समय बीत जाने के बाद भी क्या अनुच्छेद द्वारा निर्धारित समय-सीमा को बरकरार रखा जा सकता है या इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को अनुच्छेद 45 के आदेश का सम्मान करना चाहिए और इस सदी के अंत से पहले इसे वास्तविकता बनाना चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि यह वादा न केवल राज्य के विद्यालयो के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, बल्कि स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठनों को मान्यता देकर और सहायता देकर भी पूरा किया जा सकता है जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए तैयार हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि विशेष रूप से इस निर्णय में, पीठ का व्यावसायिक महाविद्यालयो को छोड़कर ऐसे निजी स्कूलों या निजी शैक्षणिक संस्थानों पर कोई टिप्पणी करने का इरादा नहीं है, क्योंकि मामले से संबंधित चर्चा मोहिनी जैन निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित थी और चुनौतियां केवल उन्हीं सिद्धांतों को दी गई थीं।
निर्णय के इस बिंदु पर, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे का उल्लेख किया है, जिसमें भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के बारे में चर्चा की गई थी। हलफनामे में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक बन गया है।
निशुल्क शिक्षा के प्रावधान पर हलफनामे में कहा गया है कि नामांकन बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सरकारी विद्यालयो में ट्यूशन शुल्क समाप्त कर दिया था और ऐसे राज्यों में निजी सहायता प्राप्त संस्थान भी अधिकतर निशुल्क थे, लेकिन निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयो की बात करें, जो देश के कुल प्राथमिक विद्यालयों का 4% हिस्सा हैं, ऐसे विद्यालयो में शुल्क लिया जाता था।
पुस्तकें, विद्यालय के कपड़े, बैग और परिवहन जैसी अन्य शैक्षिक लागतें राज्यों द्वारा वहन नहीं की जाती थीं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां गरीब परिवारों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती थी। हलफनामे में विद्यालयों द्वारा अतिरिक्त खर्च वहन न कर पाने का कारण यह बताया गया कि स्कूल का 96% व्यय शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन देने में चला जाता है।
अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान पर आते हुए हलफनामे में कहा गया है कि 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए नीतियां बनाई हैं, लेकिन कुछ सामाजिक और आर्थिक बाधाओं ने सभी छात्रों को विद्यालयों में दाखिला लेने से रोक दिया है और नियम और विनियम लागू कर दिए हैं।
हलफनामे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (सरकारी विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल) जैसे उपायों के माध्यम से उठाए गए विभिन्न कदमों का भी उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि कैसे इस तरह की पहलों ने पूरे देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है।
14 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा का अधिकार
14 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा के अधिकार पर आते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को राज्य से शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की मांग करने का अधिकार है, लेकिन इस शर्त के साथ कि यह आर्थिक क्षमता और विकास सीमाओं के भीतर होना चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि बयान का उद्देश्य अनुच्छेद 41 को संविधान के भाग IV से भाग III में स्थानांतरित करना नहीं है, बल्कि यह केवल यह साबित करने के लिए अनुच्छेद 41 पर निर्भर है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन के अधिकार से उत्पन्न होता है। न्यायालय का मानना है कि कोई भी राज्य यह राय नहीं रखेगा कि वह अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर लोगों को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता और न ही करेगा, लेकिन ऐसी सीमाएं हमेशा राज्य सरकारों की व्यक्तिपरक संतुष्टि के भीतर ही काम करती हैं।
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार केवल 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है, इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि वह 14 वर्ष की आयु के बाद अपनी आर्थिक एवं विकासात्मक सीमाओं के भीतर बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव को वैध माना और कहा कि यह प्रस्ताव नया नहीं है, यह पहले फ्रांसिस सी मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (1981) के मामले में कहा गया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि जीवन के अधिकार से विभिन्न अधिकार उत्पन्न होते हैं जैसे पोषण का अधिकार, मानव सम्मान, कपड़े, आश्रय, पढ़ने और लिखने की सुविधा, अभिव्यक्ति, स्वतंत्र रूप से घूमने आदि लेकिन ये अधिकार हमेशा राष्ट्र के विकास की सीमा पर निर्भर करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि अनुच्छेद 21 से प्राप्त शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करने के लिए निर्देशक सिद्धांतों का संदर्भ दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि भाग IV में उल्लिखित राज्य का प्रत्येक दायित्व उस संबंध में अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होने वाला अधिकार बन जाता है।
मुद्दा 3: निजी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का व्यक्तियों का अधिकार
इस कानूनी मुद्दे पर विचार करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रासंगिक अधिनियमों का विश्लेषण किया, जो इस मामले से संबंधित विभिन्न प्रकार के सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों की प्रतिव्यक्ति शुल्क, संबद्धता और मान्यता से संबंधित थे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित पहला कानून विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 था। यह अधिनियम भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानकों के समन्वय और रखरखाव के लिए संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का गठन भी हुआ।

अधिनियम में, संबद्धता को किसी महाविद्यालय के साथ संबंध या महाविद्यालय की मान्यता या महाविद्यालय के साथ जुड़ाव और प्रवेश के साथ-साथ विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम के तहत आयोग को विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयो द्वारा ली जाने वाली शुल्क को विनियमित करने का अधिकार दिया गया है।
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 को सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद के पुनर्गठन तथा भारत के लिए एक चिकित्सा रजिस्टर बनाए रखने और अन्य संबंधित मामलों के लिए कानून बनाया गया था। उक्त विधान में, “अनुमोदित संस्थान” शब्द को एक अस्पताल, एक स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे विश्वविद्यालय से एक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कोई व्यक्ति चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने से पहले आवश्यक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987
यह अधिनियम केंद्र द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (जिसे आगे ‘एआईसीटीई’ कहा जाएगा) की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि देश भर में तकनीकी शिक्षा के समन्वय, विकास और योजना को सुविधाजनक बनाया जा सके और पूरे भारत में तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा के मानकों की गुणवत्ता और रखरखाव को बढ़ावा दिया जा सके।
अधिनियम की धारा 3 में परिषद की स्थापना की गई है तथा धारा 10 में परिषद के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है। एआईसीटीई परिषद तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर लगाए जाने वाले ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्कों के संबंध में मानदंड और दिशानिर्देश तय करने, नए तकनीकी संस्थानों को मंजूरी प्रदान करने और शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय करने के लिए जिम्मेदार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि एआईसीटीई की अनुमति के बिना कोई नई तकनीकी शिक्षा संस्था स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन धारा 10 द्वारा एआईसीटीई को दी गई व्यापक शक्ति को देखते हुए, यह माना जा सकता है कि परिषद स्पष्ट उल्लेख के बिना भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, परिषद के पास मौजूदा संस्थानों में भी नए पाठ्यक्रम, संकाय और कक्षाएं शुरू करने से रोकने का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि नए संस्थानों को अनुमति प्रदान करते समय, परिषद उन्हें इस बात से अवगत कराती है कि उन्हें न केवल एआईसीटीई द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि किसी भी तरह से छात्रों से प्रतिव्यक्ति शुल्क लेने से भी बचना चाहिए। परिषद ऐसे मामलों में मान्यता या संबद्धता रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई करती है, जहां संस्थान प्रवेश के लिए छात्रों से प्रतिव्यक्ति शुल्क लेता है।
निजी शिक्षा संस्थान स्थापित करने के अधिकार से संबंधित सिद्धांत
फैसले के अगले हिस्से में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के मामलों में जमीनी हकीकत पर गौर किया। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि बजट में दूसरा सबसे अधिक व्यय शिक्षा क्षेत्र पर किया जाता है, फिर भी परिस्थितियां नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कई वैश्विक देश अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का लगभग 6-7% शिक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन भारत अपने शिक्षा क्षेत्र पर केवल 3% खर्च करता है। शिक्षा पर किये गये व्यय में से लगभग 70-80% व्यय शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर खर्च हो जाता है।
सरकारी विद्यालयो और महाविद्यालयो में शिक्षा की गुणवत्ता और मानक बनाए रखने के प्रति आत्म-अनुशासन और प्रतिबद्धता का अभाव है। मानकों में इस तरह की गिरावट के कारण निजी शिक्षा संस्थानों का निर्माण हुआ, जो जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते थे।
राज्य के पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लगातार बढ़ती मांग के लिए अधिक संसाधन समर्पित करने की स्थिति नहीं थी, इसलिए निजी शिक्षण संस्थानों ने इस कमी को पूरा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ है और निजी शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने में भी असमर्थ है, जिसके कारण केंद्र सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी और उन्हें स्थापित दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुरूप बनाया, लेकिन सरकार निजी शिक्षण संस्थानों को सरकारी शिक्षा संस्थानों के समान शुल्क लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
इन सभी विचारों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:
- सभी व्यक्तियों को सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए बिना शर्त और बिना शर्त अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह स्वयं या अन्य राज्य संस्थाओं के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करे। यह प्रस्ताव संविधान द्वारा गारंटीकृत नहीं है क्योंकि यह अवास्तविक और अव्यावहारिक है।
- निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करने से राज्य के पास अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए एजेंसी संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में एजेंसी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई परिस्थिति मौजूद नहीं होती है।
- मोहिनी जैन मामले के फैसले में दिए गए सिद्धांतों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
- निजी संस्थानों को शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा प्रदान करने से रोकना अवास्तविक एवं मूर्खतापूर्ण है। निजी संस्थानों को शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षा का व्यावसायीकरण करने से रोकने के लिए विनियामक नियंत्रण बढ़ाया जाना चाहिए। प्रभावी विनियमनों के माध्यम से शिक्षा और शैक्षिक सुविधाओं के न्यूनतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए।
- प्रवेश योग्यता के आधार पर दिए जाने चाहिए तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए जो सकारात्मक कार्रवाई के पात्र हैं। प्रवेश मानदंड पूर्व-निर्धारित एवं स्पष्ट होने चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान आवश्यक हैं और सरकार अकेले निजी संस्थानों की सहायता के बिना उच्च शिक्षा, विशेषकर चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकती। यद्यपि शिक्षा राज्य का प्राथमिक कार्य है, फिर भी वह इस विषय पर एकाधिकार नहीं रख सकता है।
निजी शिक्षण संस्थान सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों हो सकते हैं। सरकार या तो पूरी सहायता प्रदान कर सकती है या फिर परिचालन के लिए आवश्यक सहायता का एक हिस्सा प्रदान कर सकती है। सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए सरकार या संबद्धता प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, विशेषकर छात्रों के प्रवेश और कर्मचारियों की भर्ती के मामलों में कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सहायता प्राप्त संस्थाओं को सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के मामले में, उन्हें सरकारी संस्थानों के समान शुल्क लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता हैं। वे स्वेच्छा से समान शुल्क लेने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन शिक्षा प्रदान करने की अपनी लागत को पूरा करने के लिए वे अधिक शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये संस्थान स्व-वित्तपोषित और लागत-आधारित शिक्षा संस्थानों की अवधारणा पर कार्य करेंगे।
ऐसी संस्थाओं में यह प्रश्न भी उठता है कि शिक्षा की वास्तविक लागत का निर्धारण कौन करेगा तथा इसे कैसे विनियमित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा की लागत संस्थान दर संस्थान अलग-अलग हो सकती है और ऐसी लागतों का पता लगाने के लिए एक सरकारी प्राधिकरण को नामित किया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जो प्रश्न परेशान करने वाला था, वह यह था कि संवैधानिक दर्शन और संसद तथा राज्य विधानसभाओं की मंशा यह स्पष्ट करती है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण सार्वजनिक नीति के हितों के विरुद्ध है, लेकिन शिक्षा का व्यावसायीकरण किए बिना निजी संस्थानों को कैसे कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अगले कानूनी मुद्दे पर चला गया।
मुद्दा 4: शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार
सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद के खंड 6 में कहा गया है कि अनुच्छेद की कोई भी बात भारत में लागू कानून के संचालन को नहीं रोकेगी, जहां तक वह राज्य को सामान्य सार्वजनिक हित के लिए ऐसे अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार करने से रोकती है और कोई भी बात राज्य को कुछ व्यवसाय, पेशा, व्यापार और कारोबार के अभ्यास के लिए आवश्यक पेशेवर या तकनीकी योग्यता से संबंधित कानून बनाने से नहीं रोकेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उसका इस पर कोई टिप्पणी करने का इरादा नहीं है कि शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार व्यवसाय है या नहीं, लेकिन अदालत इस तथ्य से आश्वस्त है कि शिक्षा को व्यापार, व्यवसाय या पेशा नहीं माना जा सकता क्योंकि इन तीनों शब्दों में लाभ की मंशा निहित है और शिक्षा को देश में वाणिज्य वस्तु नहीं माना जा सकता है।
शिक्षा को वाणिज्य के दायरे में एकीकृत करने से न्यायालयों को आम जनता और समाज के सामाजिक लोकाचार और दर्शन के विरुद्ध जाना पड़ेगा। भारत में शिक्षा सदैव एक धार्मिक कर्तव्य रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा एक धर्मार्थ गतिविधि है, न कि कोई व्यापार या कारोबार है। शिक्षा एक पेशा या व्यवसाय न होकर एक उद्देश्य और व्यवसाय है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद की मंशा इस बात पर स्पष्ट थी कि शिक्षा का व्यावसायीकरण समाज के लिए एक बुराई है और इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यहां तक कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्य विधानसभाओं ने भी अपने-अपने अधिनियमों की प्रस्तावनाओं में शिक्षा के व्यावसायीकरण को समाप्त करने और उसे प्रस्तुत करने की मंशा व्यक्त की थी, जिसे इस विशेष मामले में सवालों के घेरे में लाया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे राज्य बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला (1957) के मामले में प्रस्तुत प्रस्ताव को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि भारत में शिक्षा को व्यापार या कारोबार नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा को वाणिज्य के रूप में नहीं समझा जा सकता है और याचिकाकर्ता शिक्षा को लाभ कमाने वाले वाणिज्य के दायरे में लाने के लिए अपने तर्क में “व्यवसाय” शब्द के व्यापक अर्थ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत निर्णयों पर विचार करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g) से प्राप्त होता है।
याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत पहला निर्णय भारत सेवाश्रम संघ बनाम गुजरात राज्य (1986) का निर्णय था, जिसमें यह माना गया था कि गुजरात माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 33 सरकार को पांच साल या उससे कम समय के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार देती है। विशिष्ट परिस्थितियों में, उपरोक्त धारा को संवैधानिक माना गया क्योंकि यह आम जनता के हित में थी और अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं थी।

इस निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय वर्तमान मामले के लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि इसमें शिक्षा को पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार मानने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम आर. राजप्पा एवं अन्य (1978) के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि शैक्षणिक संस्थान “उद्योग” शब्द के दायरे में आएंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा बयान एक अलग संदर्भ में दिया गया था और इसलिए वर्तमान मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत अगला मामला महाराष्ट्र राज्य बनाम लोक शिक्षण संस्था (1971) का मामला था, जिसमें कहा गया था कि आपातकाल की अवधि के दौरान, अन्य मौलिक अधिकारों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार पर भी रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि यह निर्णय वर्तमान मामले के लिए अप्रासंगिक है, क्योंकि निर्णय में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को ऐसा अधिकार सामान्य रूप से उपलब्ध है या नहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कहा कि शिक्षा प्रदान करने की गतिविधि को अनुच्छेद 19(1)(g) के अर्थ में पेशा नहीं कहा जा सकता है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को कभी भी “किसी पेशे का अभ्यास करने” के दायरे में नहीं लाया जा सकता जैसा कि अनुच्छेद 19(1)(g) में परिकल्पित किया गया है।
शिक्षण को एक पेशा माना जा सकता है लेकिन शिक्षा संस्थान स्थापित करना कोई पेशा नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है और यह उचित प्रतिबंधों के साथ-साथ जनता के हित के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन है।
इसके विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार के साथ संबद्धता या मान्यता का अधिकार नहीं जुड़ा है। न्यायालय ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात राज्य (1974) मामले का उल्लेख किया, जिसमें नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि भारतीय संदर्भ में संबद्धता का अधिकार मौजूद नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि संबद्धता या मान्यता के अधिकार के बिना किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अर्थहीन है।
मान्यता सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती है या सरकार द्वारा प्राप्त कोई प्राधिकारी (अथॉरिटी) द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकती है। संबद्धता किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक निकाय द्वारा प्रदान की जा सकती है जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने के लिए अधिकृत हो।
संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या निकाय को शिक्षा संस्थान स्थापित करने, कर्मचारियों की भर्ती करने, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, छात्रों को प्रवेश देने और विभिन्न पाठ्यक्रम पढ़ाने का अधिकार है, लेकिन वे यह मांग नहीं कर सकते कि उनकी डिग्री या प्रमाण पत्र को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए। कोई भी संस्था उचित प्राधिकारियों या स्वयं सरकार से मान्यता या संबद्धता प्राप्त किए बिना पर्याप्त रूप से कार्य नहीं कर सकती है।
बिना किसी मान्यता या संबद्धता के ऐसे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र और डिग्री अमान्य होंगी और छात्रों के लिए किसी काम की नहीं होंगी। कोई भी व्यक्ति ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने में रुचि नहीं लेगा, यदि अंतिम परिणाम केवल ऐसी डिग्री हो जिसका कोई मूल्य या मान्यता न हो।
यहां तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय के अलावा कोई अन्य संस्थान डिग्री प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा और यही कारण है कि निजी शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालयों से संबद्धता या मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। प्रक्रिया सरल है, जिसमें छात्रों को उन विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाता है जिनसे वे संस्थान संबद्ध होते हैं। यदि छात्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे विश्वविद्यालय से डिग्री प्रदान की जाती है।
शैक्षिक संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करते हैं तथा अध्ययन के पाठ्यक्रम भी समान होते हैं, तथा शिक्षण और प्रशिक्षण की पद्धति भी समान होती है। ये निजी शिक्षण संस्थान, भले ही संबद्ध या मान्यता प्राप्त हों, अपनी डिग्री प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि केवल छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करते हैं।
इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा प्रदान करने के राज्य के कार्य में केवल सहायता करते हैं। वे एक संबद्ध गतिविधि करते हैं, न कि राज्य से स्वतंत्र कोई विशिष्ट या पृथक गतिविधि करते हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वे कोई व्यवसाय या व्यापार कर रहे हैं।
राज्य संबद्धता या मान्यता प्रदान करते समय कुछ नियम और विनियम लागू करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत राज्य निष्पक्ष, मनमाने और उचित तरीके से मान्यता या संबद्धता प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसलिए, संबंधित हितधारकों पर शर्तें लगाए बिना निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना राज्य की ओर से गलत होगा।
यदि राज्य बिना कोई शर्त लगाए संबद्धता प्रदान करता है, तो यह उसके कर्तव्यों और दायित्वों का संवैधानिक उल्लंघन होगा, जिसके लिए वह संविधान के भाग III के आधार पर बाध्य है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य सिद्धांत को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि जो भी अधिकार, दायित्व, कर्तव्य और नियम प्राथमिक राज्य कार्य पर लागू होते हैं, वे पूरक गतिविधि पर भी लागू होने चाहिए। राज्य ऐसे दायित्वों से उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकता है और न ही वह ऐसी अनुपूरक गतिविधियां करने वालों को ऐसी उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है।
इस धारणा के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक योजना विकसित की है जिसका अनुपालन मान्यता या संबद्धता प्रदान करने वाले प्रत्येक प्राधिकारी को करना होगा। यह योजना विभिन्न राज्य अधिनियमों के सकारात्मक भागों पर आधारित थी, जिनकी इस निर्णय में चर्चा की गई थी। इस योजना की प्राथमिक अवधारणा यह थी कि संस्थान में प्रवेश के मामले में प्रबंधन के विवेकाधिकार को समाप्त किया जाए। इस विवेकाधिकार के कारण अनेक जटिलताएं उत्पन्न हुईं और यही शिक्षा के व्यावसायीकरण जैसी समस्याओं की जड़ में है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिव्यक्ति शुल्क का तात्पर्य ऐसी राशि की मांग करना है जो कानून द्वारा अनुमत राशि से अधिक है और सभी राज्य अधिनियमों में ऐसी ही परिभाषा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां प्रबंधन या उनकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य सीमा से अधिक राशि की मांग या वसूली करने की कोई संभावना न हो।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली अनुमत शुल्क, जो समान सरकारी संस्थानों द्वारा ली जाने वाली शुल्क से अधिक होती है, उसे प्रतिव्यक्ति शुल्क नहीं कहा जा सकता है। सभी राज्य अधिनियम निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा उच्च शुल्क वसूलने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन वे केवल उनके द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क को विनियमित करते प्रतीत होते हैं, जिसे अनुमत शुल्क कहा जाता है, तथा उन्हें अनुमत स्तर से अधिक कुछ भी वसूलने से रोकते हैं, जिसे प्रतिव्यक्ति शुल्क कहा जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजी शिक्षण संस्थानों के लिए योजना/दिशानिर्देश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित योजना दिशा-निर्देशों की प्रकृति की थी, जिसे उपयुक्त सरकार और संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा शर्तें लगाते हुए मान्यता दी जा सकती थी। योजना में कहा गया था कि:
- व्यावसायिक महाविद्यालयो की स्थापना और प्रबंधन केवल पंजीकृत सोसायटी, सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) या धार्मिक एवं धर्मार्थ निकाय द्वारा ही की जा सकेगी। किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य निकाय को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो मौजूदा शिक्षण संस्थान ऐसे मानदंडों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें छह महीने के भीतर इनका अनुपालन करने को कहा गया।
- सभी व्यावसायिक महाविद्यालयो में न्यूनतम 50% सीटें सरकारी या विश्वविद्यालय के नामांकितों द्वारा भरी जाएंगी और उन्हें निःशुल्क सीटें कहा जाएगा। योग्यता के आधार पर चुने गए विद्यार्थियों को ऐसी सीटों पर प्रवेश दिया जाना था तथा प्रवेश प्राधिकारियों द्वारा मानदंड तय किए जाने थे। शेष 50% सीटों के लिए भुगतान आमंत्रित किया जाना था, जिन्हें निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना था। प्रबंधन कोटा में कोई आरक्षण की अनुमति नहीं थी। दोनों सीटों के लिए पात्रता के मानदंड समान होंगे तथा एकमात्र अपवाद उच्च शुल्क का भुगतान करने की इच्छा होगी। व्यावसायिक महाविद्यालयो के प्रबंधन को दोनों प्रकार की सीटों के लिए कोई अन्य पात्रता मानदंड लागू करने की अनुमति नहीं थी।
- किसी व्यावसायिक महाविद्यालय में सीटों की संख्या समुचित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा ऐसे प्राधिकारियों की अनुमति के बिना इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती है।
- विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश के लिए अलग से आवेदन नहीं मांगे जा सकेंगे। केवल सक्षम प्राधिकारी ही प्रवेश के लिए निर्णय ले सकता है।
- प्रत्येक व्यावसायिक महाविद्यालय को अनुशंसित शुल्क संरचना अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी तथा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य सरकार को व्यावसायिक महाविद्यालयो द्वारा ली जाने वाली शुल्क की अधिकतम सीमा तय करने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए।
यह योजना शैक्षणिक वर्ष 1993-94 से लागू की गई।
मामले का महत्व
इस मामले में निर्णय काफी व्यापक है क्योंकि इसमें भारत के विभिन्न राज्यों, कई महत्वपूर्ण कानूनों और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों की व्याख्या से संबंधित मामलों पर विचार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा के अधिकार के अस्तित्व तथा 14 वर्ष की आयु तक सभी नागरिकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के राज्य के दायित्व को मान्यता दी गई है।
14 वर्ष की आयु के बाद, राज्य का दायित्व उसके आर्थिक साधनों और विकास पर निर्भर करता है। इसने मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले ऐतिहासिक निर्णय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को भी पलट दिया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया, जिसने सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा के अधिकार की स्पष्ट रूप से गारंटी दी है।
इस निर्णय में यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया कि मौलिक अधिकार और राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए, यह निर्णय भारतीय न्याय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा एक मूल्यवान मिसाल है।

निष्कर्ष
यह मामला शिक्षा के अधिकार और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के अधिकार के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्माण करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय था। हालांकि फैसले का पाठ व्यापक है, लेकिन इसमें राष्ट्रीय नीति को बरकरार रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का व्यावसायीकरण जनता की नैतिकता और हितों के खिलाफ है। यह शिक्षा के महत्व को स्वीकार करता है, साथ ही शिक्षा प्रदान करने के प्रति राज्य के दायित्व के महत्व को भी स्वीकार करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णय द्वारा किन मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई?
इस निर्णय में कुछ सीमाओं के साथ शिक्षा के मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई तथा बिना किसी अधिकार के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के मौलिक अधिकार को भी मान्यता दी गई, जो उक्त संस्थान के लिए संबद्धता या मान्यता की गारंटी देता हो।
शिक्षा के अधिकार पर क्या सीमाएं लगाई गई हैं?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है तथा इस आयु के बाद यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के अधीन है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रतिव्यक्ति शुल्क की परिभाषा क्या है?
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर-सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को अपने व्यय को पूरा करने के लिए उच्च शुल्क की आवश्यकता होती है और ऐसा शुल्क एक समिति द्वारा तय किया जाएगा, लेकिन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक ली जाने वाली राशि को प्रतिव्यक्ति शुल्क कहा जाएगा।
क्या अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत शिक्षा प्रदान करना एक व्यवसाय, कारोबार या पेशा है?
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, शिक्षा प्रदान करना अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत किसी भी शर्त के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने में लाभ की मंशा नहीं जोड़ी जा सकती है।
संदर्भ