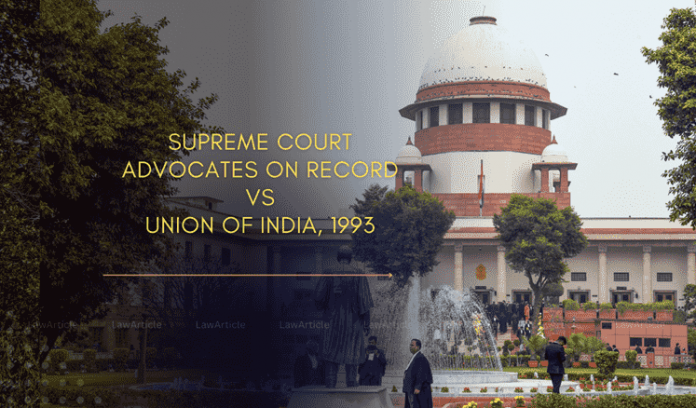यह लेख प्रशांत गुप्ता द्वारा लिखा गया है और Syed Owais Khadri द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया है । यह लेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (1993) में दिए गए फैसले का व्यापक अध्ययन प्रदान करता है। यह तथ्यों, तर्कों, निर्णय और तर्क पर विस्तार से चर्चा करता है। यह मामले में शामिल कानून के बिंदु पर भी प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, लेख निर्णय का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने का भी प्रयास करता है। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
हाल के दिनों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच काफी मतभेद देखने को मिले हैं। न्यायपालिका जहां कार्यपालिका द्वारा अनुशंसित (रिकमेंड) नामों की न्यायिक नियुक्तियां करने में कार्यपालिका के विलंब या उसकी अवज्ञा से नाखुश है, वहीं कार्यपालिका अपनी कार्रवाई जारी रखने पर अड़ी हुई है। दरअसल, कार्यपालिका ने कॉलेजियम प्रणाली की बहुत आक्रामक तरीके से आलोचना या उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। कानून मंत्री द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को संविधान के लिए एक विदेशी अवधारणा बताते हुए की गई टिप्पणी ने इस संबंध में एक नई बहस शुरू कर दी है। कार्यपालिका के अन्य सदस्यों द्वारा भी इसी तरह के बयान दिए गए।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह विभिन्न मामलों में न्यायिक मिसालों के माध्यम से विकसित हुई है। कॉलेजियम प्रणाली पहली बार सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (1993) के मामले के बाद स्थापित की गई थी और बाद में तीसरे न्यायाधीश के मामले में इसे प्रबल (स्ट्रेंथन) किया गया था। यह लेख ऊपर उल्लिखित मामले पर चर्चा करता है जिसके कारण कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई।
यह मामला न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों पर पुनर्विचार के लिए एक दलील थी जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में अपने द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया था । इसने “न्यायपालिका की अखंडता की रक्षा और स्वतंत्रता की रक्षा” के हित में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया भी तैयार की, जिसे अब कॉलेजियम प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसी कारण से, भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता आवश्यक मानी गई थी। यह मामला संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आधारित है। यह मामला ‘द्वितीय न्यायाधीश मामला’ के रूप में प्रसिद्ध है। ‘कानून के शासन’ को सुरक्षित करने के लिए जो लोकतांत्रिक प्रणाली के संरक्षण के लिए आवश्यक है और शक्तियों का पृथक्करण (सेपरेशन) जिसे संविधान में ‘न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने’ के निर्देशक सिद्धांतों के साथ अपनाया गया है।
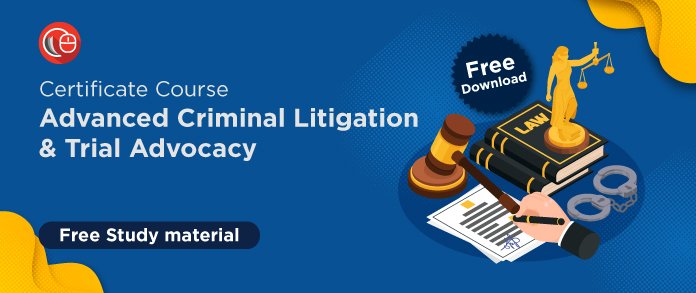
मामले का विवरण
इस लेख में चर्चित मामले के कुछ महत्वपूर्ण विवरण निम्नलिखित हैं-
-
- मामले का नाम: सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ (1993) (इसके बाद इसे लेख में “तत्काल केस” के रूप में संदर्भित किया गया हैं)
- मामला संख्या: रिट याचिका 1303/1987 (रिट याचिका 156/1993 के साथ)
- मामले के पक्षकार:
-
- याचिकाकर्ता: सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य।
- प्रतिवादी(गण): भारत संघ।
- समतुल्य उद्धरण: ए आई आर 1994 एस सी 268, (1993) 4 एस सी सी 441
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- पीठ: जस्टिस. एस रत्नावेल पांडियन, एएम अहमदी, कुलदीप सिंह, जेएस वर्मा, एमएम पुंछी, योगेश्वर दयाल, जीएन रे, डॉ. एएस आनंद और डॉ. एसपी भरूचा।
- निर्णय की तिथि: 6 अक्टूबर, 1993
- निर्णय का अनुपात: 7 (5 बहुमत + 2 सहमति): 2 (असहमति)
मामले की पृष्ठभूमि
न्यायपालिका की नियुक्ति से संबंधित मामले संविधान की स्थापना के बाद से ही न्यायिक मन को परेशान और उलझन में डालते रहे हैं। इस मामले को न्यायपालिका की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करके सुलझाया जाना चाहिए। एक अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक संस्था के लोकतांत्रिक नियंत्रण और निष्पक्ष मध्यस्थता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ा।
यह मामला सांकल चंद बनाम भारत संघ (1976) में निर्णय के लिए आया , जहां अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण को बरकरार रखा। हालांकि, 1982 तक, यह बहस महाकाव्य अनुपात तक पहुंच गई थी। इन मामलों ने न्यायाधीशों के स्थानांतरण के कदम पर सवाल उठाने वाली रिट याचिकाओं के एक समूह में ठोस रूप ले लिया, जिसमें कुछ न्यायाधीशों के प्रभावित स्थानांतरण को चुनौती दी गई और न्यायाधीशों की संख्या की औचित्य (जस्टिफायबिलिटी) की मांग की गई।
इन मुद्दों का विकास एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) के मामले से शुरू हुआ और इसके बाद सुभाष शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ (1990) आया, जहां इसे अंततः एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया, जो कि तत्काल मामला है। मुद्दों या मामले के विकास पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982)
- यह मामला केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती देने से संबंधित था, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्धारित की गई थी।
- नियुक्तियों को निर्धारित करने वाले परिपत्र की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं।
- इस बीच, कुछ न्यायाधीशों के तबादले का आदेश भी जारी किया गया। तबादले के आदेशों की संवैधानिक वैधता को भी रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई।
- ये सभी याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 139A के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दी गईं ।
- इसके अतिरिक्त, स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और इसी संबंध में एक अन्य विशेष अनुमति याचिका भी दायर की गई थी।
- इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री एस.पी गुप्ता द्वारा दायर रिट याचिका को मुख्य याचिका के रूप में रखते हुए एक संविधान पीठ का गठन करके सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया।
- इस मामले में संवैधानिक महत्व के कई सवाल शामिल थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित था। इस मामले में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे तैयार किए गए और उन पर निर्णय सुनाया गया। हालाँकि, इस मामले में ध्यान देने योग्य दो मुख्य मुद्दे ये हैं,
- न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता; और
- न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता।
इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित प्रावधानों में उल्लिखित अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों पर राय की प्राथमिकता प्राप्त नहीं है। न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया था कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए सरकार/कार्यपालिका को आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इसने माना कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का मामला ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा के माध्यम से तय किया जा सके।
सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ (1990)
एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में ऊपर बताए गए दो मुद्दों के संबंध में दिए गए निर्णय के बाद आलोचना और विवाद हुआ और फिर अंततः विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए तीन रिट याचिकाएँ दायर की गईं। इनमें से एक याचिका श्री सुभाष शर्मा द्वारा दायर की गई थी और एक सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी और इसी संबंध में एक और याचिका भी थी। तीनों याचिकाओं को सुभाष शर्मा द्वारा मुख्य याचिका के तहत सुभाष शर्मा बनाम भारत संघ (1990) के रूप में शामिल किया गया था ।
इस मामले में न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में शेष रिक्तियों को समय पर दाखिल करने के बारे में महान्यायवादी द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद पहली और अंतिम याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि, दूसरी याचिका को ऊपर उल्लिखित दो प्रमुख मुद्दों की जांच या पुनर्विचार के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया गया। इस संदर्भ के कारण अंततः यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पहुंचा।

मामले के तथ्य
वर्तमान मामला न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक महत्व के मुद्दों की जांच के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष था। इस मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लाने वाले मुद्दों के तथ्यों और पृष्ठभूमि पर फिर से गौर करना और ध्यान देना महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
- यह याचिका 1987 में सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए दायर की गई थी। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील सुभाष शर्मा द्वारा भी इसी राहत के लिए प्रार्थना करते हुए एक और जनहित याचिका दायर की गई थी।
- तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्री सुभाष शर्मा द्वारा सुभाष शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ (1990) में दायर जनहित याचिका पर विचार करते समय इस याचिका पर गौर किया। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक आदेश पारित किया, जिसमें उक्त मामले के साथ-साथ इस याचिका और अन्य संबंधित मामलों को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
- मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया संदर्भ ऊपर उल्लिखित तत्काल मामले में शामिल मुद्दों की जांच के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ के गठन के लिए था। उक्त मामलों में न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक महत्व के मुद्दे शामिल थे और इसलिए इसे एक बड़ी पीठ को भेजा गया था।
- रेफरिंग पीठ (तीन न्यायाधीशों की पीठ) ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि उसका मानना था कि एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में बहुमत के दृष्टिकोण से दिए गए निर्णय की सत्यता के लिए एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। तीन न्यायाधीशों की पीठ के आदेश के अनुसार कानून के मुख्य प्रश्न या जिन मुद्दों पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी, उनका उल्लेख नीचे किया गया है।
- हालांकि, इस मोड़ पर, संविधान (67वां संशोधन) विधेयक, 1990 संसद में पेश किया गया जिसमें अनुच्छेद 124(2), 217(1), 222(1) और 231 (2) (A) में संशोधन करने की मांग की गई। यह विधेयक राष्ट्रपति को राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के रूप में ज्ञात एक न्यायिक आयोग स्थापित करने का अधिकार देने के लिए लाया गया था। घोषित उद्देश्य 121वें विधि आयोग की रिपोर्ट को लागू करना था। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि न्यायपालिका की नियुक्ति की देखरेख के लिए एक न्यायिक आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। हालांकि, इसका कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि 9वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया। एस.पी गुप्ता मामले की समीक्षा की मांग करने वाली रिट याचिकाओं की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा और न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया और एमएम पुंछी शामिल थे, जिन्होंने पुनर्विचार की सिफारिश की।
उठाए गए मुद्दे
यद्यपि इस मामले में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का पृथक्करण, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के कार्य, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों से सहायता और सलाह, सिफारिश और परामर्श जैसे विभिन्न शब्दों की व्याख्या से संबंधित विभिन्न प्रश्न शामिल थे, लेकिन बहुमत के फैसले देने वाले न्यायाधीशों द्वारा दो मुद्दों को प्राथमिक मुद्दों के रूप में तैयार किया गया। निर्णय के लिए तैयार किए गए मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं।
- क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई राय अन्य पदाधिकारियों की राय पर प्राथमिकता रखती है या नहीं?
- क्या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण के मामले सहित ऐसे मामले न्यायोचित हैं?
इसमें शामिल कानूनी मुद्दा
किसी भी मामले में मुद्दों से संबंधित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों को समझना ऐसे मुद्दों के उचित विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले में चर्चा या जांच किए गए प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों पर नीचे चर्चा की गई है।
भारत का संविधान
वर्तमान मामला न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक प्रक्रियाओं या मामलों आदि में कार्यपालिका या संसद की भागीदारी के मुद्दे के इर्द-गिर्द घूमता है। वर्तमान मामले में उल्लिखित भारतीय संविधान के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं।
संविधान का अनुच्छेद 12
संविधान का अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रावधान है क्योंकि यह “राज्य” की परिभाषा निर्धारित करता है, जिसमें यह परिभाषित किया गया है कि “राज्य” शब्द में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।
यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन प्राधिकारियों को निर्धारित करता है जिनके विरुद्ध संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है या जिन प्राधिकारियों पर मौलिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का कर्तव्य अधिरोपित (इंपोस्ड) किया गया है।
इस प्रावधान के तहत “राज्य” की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 36 के अनुसार संविधान के भाग IV के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर भी लागू होती है।
माननीय न्यायालय ने इस मामले में अनुच्छेद 36 के तहत प्रावधान पर गौर किया और कहा कि यह परिभाषा पूरे भाग IV पर लागू होती है और इसलिए अनुच्छेद 50 में “राज्य” की व्याख्या वितरणात्मक (डिस्ट्रीब्यूटीव) अर्थ में की जानी चाहिए ताकि इसकी परिभाषा में उल्लिखित सभी प्राधिकरणों जैसे कि सरकार, स्थानीय और भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी अन्य प्राधिकरणों को शामिल किया जा सके। तदनुसार, इसने आगे कहा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की अवधारणा की जांच उच्च न्यायपालिका की उपेक्षा करते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका तक सीमित नहीं की जा सकती।
संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368
दोनों प्रावधानों पर एक साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और संवैधानिक कानून के परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) से बहुत महत्वपूर्ण हैं।
संविधान का अनुच्छेद 13
संविधान का अनुच्छेद 13 ऐसे किसी भी ‘कानून’ को अमान्य घोषित करता है जो संविधान के भाग III का उल्लंघन करता है। यह राज्य को ऐसे ‘कानून’ बनाने से भी रोकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या उन्हें छीनते हैं और अगर बनाए जाते हैं, तो ऐसे कानून इस प्रावधान के तहत अमान्य होंगे।
हालाँकि, इस अनुच्छेद के खंड (4) में अमान्यता के लिए अपवाद दिया गया है। अनुच्छेद 13(4) में प्रावधान है कि यदि कानून संविधान के भाग III का उल्लंघन करते हैं तो उनकी अमान्यता का नियम संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधनों पर लागू नहीं होगा ।
इसके अलावा, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अनुच्छेद 13(3)(A) , जो “कानून” शब्द को परिभाषित करता है, अपनी परिभाषा के भीतर संशोधन को शामिल नहीं करता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त उप-खंड के तहत प्रदान की गई परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है न कि संपूर्ण।
संविधान का अनुच्छेद 368
अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़ने, निरस्त करने या बदलने के लिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 368(3) अनुच्छेद 13(4) के प्रावधान के समान है। यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनों के लिए अनुच्छेद 13 के तहत नियम के आवेदन से छूट देता है।
संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन करने के लिए संसद द्वारा प्रदत्त शक्ति के दायरे के संबंध में अनिश्चितता और स्पष्टता की कमी के कारण उक्त संवैधानिक मुद्दे पर महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई।
बुनियादी संरचना (बेसिक स्ट्रक्चर) अवधारणा
इस संवैधानिक मुद्दे पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) , सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964) , और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) सहित विभिन्न निर्णयों में लंबे समय तक बहस हुई , और अंततः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में ऐतिहासिक निर्णय में इसका समाधान हुआ, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
मूल संरचना सिद्धांत में बस इतना कहा गया है कि संसद को संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे संशोधन संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे समानता, न्याय आदि के विरोधाभासी या उल्लंघन में नहीं होने चाहिए। यह उन सिद्धांतों की विस्तृत सूची प्रदान नहीं करता है जिन्हें संविधान के लिए मौलिक माना जाना चाहिए, लेकिन सिद्धांत के तहत क्या शामिल किया जा सकता है, इसका एक व्यक्तिपरक विचार प्रदान करता है। यह मूल रूप से संविधान की भावना को संदर्भित करता है।

संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226
ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये व्यक्तियों के अधिकारों के प्रवर्तन या संरक्षण के लिए एक तंत्र (मैकेनिज्म) या उपाय प्रदान करते हैं। जबकि पहला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ऐसा तंत्र प्रदान करता है, दूसरा राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों के समक्ष ऐसा करता है।
संविधान का अनुच्छेद 32
संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। यह अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में रिट याचिका दायर करके सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने के अधिकार की गारंटी देता है।
संविधान का अनुच्छेद 226
अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त शक्तियों के समान शक्तियाँ प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का उपाय प्रदान करता है। संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति इस प्रावधान के तहत अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए माननीय उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस प्रावधान का दायरा संविधान के अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है। अनुच्छेद 32 के विपरीत अनुच्छेद 226 अपने दायरे को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित नहीं रखता है बल्कि इससे आगे तक विस्तारित करता है। इस प्रावधान का खंड 1 “ भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए ” वाक्यांश के साथ समाप्त होता है । ‘किसी अन्य उद्देश्य’ शब्दों को अनुच्छेद 32 के तहत शामिल नहीं किया गया है, जो इस प्रावधान के दायरे को अनुच्छेद 32 से व्यापक बनाता है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकता है, जो अनुच्छेद 32 के तहत संभव नहीं है। इसके अलावा, अनुच्छेद 226 खुद को ‘राज्य’ तक सीमित नहीं करता है। खंड 1 में स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय, इस प्रावधान के तहत किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ रिट जारी करने की शक्ति रखता है।
संविधान का अनुच्छेद 50
अनुच्छेद 50 , संविधान के भाग IV के अंतर्गत आता है जिसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इस प्रावधान में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लेख है। यह प्रावधान न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके इस अवधारणा को लागू करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य लगाता है। यह राज्य से राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उपाय करने का आह्वान करता है।
न्यायपालिका की स्थापना, गठन और नियुक्तियों से संबंधित प्रावधान
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्थापना और संरचना तथा इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की गई है।
- अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में प्रावधान करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और हटाने से संबंधित प्रावधान हैं।
- इस प्रावधान के खंड 2 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
- खंड 3 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं।
- खंड 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण और मतदान के बाद न्यायाधीश को हटाया जाएगा।
- अनुच्छेद 126 और 127 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 223 और 224 में राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों और अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय निर्धारित करता है तथा अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों की संरचना निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 217 में राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसमें उनकी योग्यताओं से संबंधित प्रावधान भी हैं और यह भी प्रावधान है कि हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 121(4) में उल्लिखित प्रक्रिया के समान होगी।
- अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है।
नोट: मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नियुक्तियाँ और स्थानांतरण राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संस्तुति पर किए जाने हैं, लेकिन जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, तब ऐसे प्रावधानों में यह प्रावधान था कि ऐसी नियुक्तियाँ और स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श से किए जाएँगे, यदि आवश्यक समझा जाए। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संस्तुति की आवश्यकता 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा डाली गई थी, लेकिन बाद में इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (2015) में रद्द कर दिया था ।
- अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाने का प्रावधान है। यह जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता भी प्रदान करता है। इसमें प्रावधान है कि नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर की जाएगी।
उपर्युक्त सभी प्रावधान न्यायिक मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका को प्रतिबिंबित करते हैं, जो शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा से हटकर है।
अन्य संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह दे, जो ऐसी सलाह के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है। इसी तरह, अनुच्छेद 163 में राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में) का कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह राज्यपाल को सहायता और सलाह दे।
- अनुच्छेद 112 में भारत की संचित निधि के वार्षिक वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रावधान हैं और अनुच्छेद 113 में पिछले प्रावधान में उल्लिखित ऐसी निधियों के अनुमानों से संबंधित संसद में प्रक्रिया का प्रावधान है। इसी तरह, अनुच्छेद 202 में प्रत्येक राज्य की संचित निधि के वार्षिक वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रावधान हैं और अनुच्छेद 203 में पिछले प्रावधान में उल्लिखित ऐसी निधियों के अनुमानों से संबंधित राज्य विधानमंडलों में प्रक्रिया का प्रावधान है।
अनुच्छेद 112(3)(d) और अनुच्छेद 202(3)(d) भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों के न्यायाधीशों को पारिश्रमिक, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का भुगतान निर्धारित करते हैं।

- अनुच्छेद 121 संसद में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने पर रोक लगाता है। हालाँकि, उक्त प्रतिबंध का एक अपवाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को संबोधित प्रस्ताव है। इसी तरह, अनुच्छेद 211 किसी भी राज्य विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर किसी भी चर्चा पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 125 और 221 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान निर्धारित करते हैं।
- अनुच्छेद 129 और 215 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हैं।
- अनुच्छेद 136 , 137 और 145 सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करते हैं, जैसे विशेष अनुमति देने की शक्ति, निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति, तथा न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति आदि।
- अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए या घोषित कानून को अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाता है।
पक्षों के तर्क
विभिन्न वकीलों द्वारा अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए। मुख्य विषय संविधान के अनुच्छेद 74, 124 और 217 के तहत सलाहकार शक्तियों का दायरा और सीमा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों का पृथक्करण, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में उल्लिखित परामर्श शब्द का अर्थ, विभिन्न पदाधिकारियों के बीच सलाह की प्रधानता और न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण और न्यायसंगतता से संबंधित थे। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों दोनों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर संक्षेप में इस प्रकार चर्चा की गई है।
याचिकाकर्ता
इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में कई प्रतिष्ठित वकीलों ने दलीलें पेश कीं, लेकिन मुख्य दलीलें याचिकाकर्ता श्री एस.पी गुप्ता और श्री फली एस नरीमन और श्री कपिल सिब्बल ने पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि जिस मुख्य मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए दलीलें दी जा रही हैं, वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त, श्री राम जेठमलानी ने एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार के लिए छह कारण बताए जो इस प्रकार हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों पर ध्यान न देना।
- संविधान की व्याख्या के लिए लागू व्याख्या के सिद्धांत वे थे जो क़ानूनों के लिए भी मान्य थे।
- अनुच्छेद 124 और 217 के तहत राष्ट्रपति के बारे में गलत धारणा अनुच्छेद 74 के तहत भी वैसी ही है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस आधार पर प्राथमिकता देने से गलत तरीके से इनकार किया गया कि न्यायपालिका जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है क्योंकि यह एक गैर-निर्वाचित पद है।
- संविधान सभा के सदस्यों के भाषणों के रूप में अस्वीकार्य सामग्री पर निर्भरता।
- यह निर्णय लापरवाही के साथ लिया गया था ।
याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तर्क निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत थे।
न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित प्रावधानों पर संविधान की मूल विशेषताओं का प्रभाव
- याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि संविधान की मूल विशेषताएं, जिनमें अनुच्छेद 124(2) और 217(1) शामिल हैं, न्यायिक नियुक्तियों और न्यायिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में अनुच्छेद 74 के दायरे को सीमित करती हैं।
- याचिकाकर्ताओं ने संविधान की मूल विशेषताओं के रूप में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिलाया:
- अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत प्रावधान न्यायिक प्राधिकारियों या पदाधिकारियों की प्रभावी, स्वतंत्र और सकारात्मक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।
- न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं सरकार की अन्य शाखाओं के प्रभाव से पूर्णतः पृथक करना।
- अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, तथा संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका की स्वतंत्रता या पृथक्करण।
- उन्होंने यह भी तर्क दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल नियुक्ति के बाद ही लागू नहीं होती, बल्कि इसमें न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया भी शामिल है।
- उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के संबंध में डॉ. बी.आर अंबेडकर द्वारा दिए गए एक बयान की ओर भी ध्यान दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि “न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और अपने आप में सक्षम होना चाहिए”।
- इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 271(1) में उल्लिखित राज्यपाल से परामर्श संविधान की मूल विशेषता नहीं है।
- उन्होंने अंततः तर्क दिया कि संविधान के मूल प्रावधान मुख्य संवैधानिक ढांचे के अनुरूप प्रावधानों के दायरे को सीमित करते हैं। इसके अलावा, यदि दो संवैधानिक प्रावधानों के बीच कोई संघर्ष है, तो उन प्रावधानों की व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो संविधान के मूल सिद्धांतों या ढांचे के अनुरूप हो।
अनुच्छेद 74(1), 124(2) और 217(1) के तहत प्रावधानों की पेचीदगियां
- याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अनुच्छेद 74(1) मंत्रिपरिषद के दो कार्य निर्धारित करता है, जिनमें से एक न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में लागू नहीं होता है क्योंकि इसे अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत न्यायिक पदाधिकारियों को सौंप दिया जाता है। मंत्रिपरिषद के दो कार्य इस प्रकार हैं।
- सलाहकार कार्य अर्थात राष्ट्रपति को सलाह देना; और
- सूचनात्मक कार्य, अर्थात राष्ट्रपति की सहायता करना।
- तदनुसार, न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में, अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत उल्लिखित सिफारिश या परामर्श केवल न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा दिए जाने तक ही सीमित है। इसके अलावा, ऐसी सिफारिश या परामर्श अनुच्छेद 74(1) के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह के दायरे को सीमित करता है।
- सरल शब्दों में, इन तीनों प्रावधानों के बीच परस्पर क्रिया यह है कि न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में, अनुच्छेद 74(1) के तहत उल्लिखित “सलाह” को अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत “न्यायिक पदाधिकारियों के साथ सिफारिश/परामर्श” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसलिए, न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में, अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का एकमात्र कर्तव्य या कार्य राष्ट्रपति को केवल “सहायता” तक सीमित है क्योंकि सलाहकार कार्य न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
- उन्होंने तर्क दिया कि मंत्रिपरिषद के सलाहकारी कार्यों का बहिष्कार या प्रतिबंध कार्यपालिका के प्रभाव से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए था।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि अनुच्छेद 124 के तहत प्रावधान की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान न्यायाधीशों से परामर्श की आवश्यकता जानबूझकर की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 124(2) के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श अनिवार्य है।
परामर्श का अर्थ और मुद्दा
- याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि संवैधानिक प्राधिकारियों अर्थात न्यायिक पदाधिकारियों के साथ परामर्श की विचारपूर्वक आवश्यकता, न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए संवैधानिक आधारों में से एक है।
- उन्होंने तर्क दिया कि “परामर्श” शब्द में सलाह भी शामिल है और इसका तात्पर्य सलाह से है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जिस व्यक्ति से परामर्श किया जाना चाहिए या जिसके लिए बाध्य किया जाना चाहिए, उसके द्वारा दी गई सलाह नियुक्ति प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी है।
- उन्होंने तर्क दिया कि उपरोक्त आवश्यकता का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सबसे उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान को सुगम बनाना था, न कि ऐसे व्यक्तियों की जो केवल ऐसी नियुक्तियों के लिए योग्य हैं। ऐसी पहचान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी से बेहतर जानता हो, जो इस मामले में स्वयं न्यायिक पदाधिकारी हैं।
- उन्होंने तर्क दिया कि परामर्श करने का दायित्व नियुक्ति की शक्ति के साथ इस तरह एकीकृत है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट (स्पेसिफिक) व्यक्तियों के साथ परामर्श के कर्तव्य के प्रदर्शन के साथ ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस तरह का एकीकरण परामर्श निर्धारित करने वाले प्रावधानों में परिलक्षित होता है।
- इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत प्रावधान केवल संवैधानिक प्राधिकारियों को निर्धारित करते हैं जिनसे नियुक्तियों की प्रक्रिया के दौरान परामर्श किया जाना है। हालाँकि, ये प्रावधान परामर्श या उपयुक्त उम्मीदवारों की बाद की सिफारिश के लिए कोई विधि या प्रक्रिया निर्धारित नहीं करते हैं। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए ऐसी सिफारिशों को न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए और कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए।
- अंततः, उन्होंने तर्क दिया कि नियुक्तियों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करने का अधिकार केवल न्यायिक पदाधिकारियों के पास होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अन्य सभी संवैधानिक अधिकारियों से इस तरह से परामर्श किया जाना चाहिए जिससे निम्नलिखित कार्य सुगम हो सकें।
- न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना।
- यह सुनिश्चित करना कि अंतिम रूप से केवल न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसित व्यक्ति ही नियुक्त किए जाएं।
प्राथमिकता का प्रश्न/मुद्दा
- याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित कोई भी प्रावधान, खास तौर पर अनुच्छेद 124(2) और 271(1) उन प्रावधानों में उल्लिखित संवैधानिक अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह की प्रधानता का संकेत नहीं देते हैं। उन्होंने दलील दी कि ऐसी प्रधानता न्यायपालिका की कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुसार तय की जानी चाहिए।
- उन्होंने मुख्य रूप से तर्क दिया कि प्राथमिकता के प्रश्न का उत्तर मंत्रिपरिषद पर न्यायिक पदाधिकारियों की प्राथमिकता के रूप में समझा जाना चाहिए। ऐसी प्राथमिकता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, न कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिकता।
- उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की भूमिका केवल सहायता प्रदान करने की है, इसलिए परामर्श के लिए एकमात्र प्राधिकारी न्यायिक पदाधिकारी हैं। इसलिए प्राथमिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भले ही मंत्रिपरिषद की सलाहकार भूमिका मानी जाती हो, लेकिन उनके द्वारा दी गई ऐसी सलाह न्यायिक पदाधिकारियों की सलाह के अनुरूप होनी चाहिए या न्यायिक पदाधिकारियों की सलाह को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- इसके अलावा, यह भी कहा गया कि न्यायिक पदाधिकारियों के भीतर, मुख्य न्यायाधीश को उनके द्वारा दी गई सलाह का अंतिम प्रवक्ता माना जाना चाहिए, क्योंकि वह भारतीय न्यायिक पदाधिकारियों के प्रमुख हैं।

न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 216 राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में निर्णय लेने के लिए व्यक्तिपरक विवेकाधिकार की अनुमति नहीं देता है। यह राष्ट्रपति पर लंबित मुकदमों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का दायित्व डालता है। राष्ट्रपति समय-समय पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर विचार करते हुए ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य है।
- उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 16 के तहत “समय-समय पर नियुक्ति करना आवश्यक समझा जा सकता है” शब्द राष्ट्रपति पर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की निरंतर समीक्षा या पुनर्विचार करने के दायित्व को दर्शाता है।
- उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 216 के तहत प्रावधान की व्याख्या करते समय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई और न्याय के अधिकार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह की व्याख्या राज्य पर एक मौलिक कर्तव्य डालती है कि वह उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की निरंतर समीक्षा और पुनर्विचार करे ताकि शीघ्र सुनवाई और न्याय सुनिश्चित हो सके।
- याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधीशों की संख्या की न्यायसंगतता के मुद्दे से संबंधित एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दी, जिसमें इस मुद्दे को न्यायसंगत नहीं माना गया था।
प्रतिवादी
मुख्य तर्क भारत के महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में माननीय न्यायमूर्ति पाठक के विचारों को स्वीकार करने का प्रस्ताव देकर एक मध्य मार्ग सुझाया। श्री के. परासरन, जो भारत संघ की ओर से बहस कर रहे थे, ने एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में दिए गए बहुमत के मत की पुष्टि के लिए तर्क दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण तर्क इस प्रकार थे।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल्यांकन या चर्चा करते समय सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, उच्च न्यायपालिका को उससे संबंधित सेवा शर्तों और प्रक्रियाओं के बारे में कड़े प्रावधानों द्वारा संरक्षित किया जाता है।
- उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्य है और कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है। नतीजतन, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति भी उनके पास है। हालाँकि, ऐसी शक्ति संवैधानिक अधिकारियों के साथ परामर्श को अनिवार्य करने वाले कुछ प्रावधानों द्वारा विनियमित है।
- उन्होंने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उन राज्यों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है।
- उन्होंने तर्क दिया कि संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता का भी प्रावधान है। फिर भी, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया न्यायाधीशों की नियुक्ति के समान ही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। तदनुसार, उन्होंने तर्क दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन पर आधारित हो।
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि सरकार की एक अलग शाखा या एक अलग संवैधानिक प्राधिकरण में नियुक्ति शक्ति के अस्तित्व का तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हुई है।
- उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली पर आधारित है, जहां न्यायिक नियुक्तियां कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अब तक इतनी अच्छी तरह से काम करने वाली प्रणाली को बदलना अनुचित है।
परामर्श का अर्थ और मुद्दा
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि “परामर्श” शब्द का अर्थ “सिफारिश”, “सहमति” या “सहायता और सलाह” के समान नहीं है।
- उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 233 के तहत एक ही प्रावधान में दो अलग-अलग शब्दों सिफारिश और परामर्श का एक साथ इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक ही प्रावधान में अलग-अलग शब्दों के इस्तेमाल से यह स्पष्ट हो जाता है कि अलग-अलग शब्दों का चयन जानबूझकर किया गया था।
- उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत “परामर्श” शब्द एक प्रभावी अर्थ प्रदान करता है और विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान को व्यक्त करता है।
- प्रतिवादियों ने जोर देकर कहा कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि इस्तेमाल की गई अभिव्यक्तियों की भाषा का उल्लंघन हो। इसके अलावा, इसकी व्याख्या इस तरह से भी नहीं की जा सकती कि इस्तेमाल किए गए शब्दों को कोई विरोधाभासी अर्थ मिले।
प्राथमिकता (प्राइमेसी) का प्रश्न/मुद्दा
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि संवैधानिक प्राधिकारियों में से किसी एक की प्रधानता का प्रश्न परामर्श की अवधारणा के साथ असंगत है। हालांकि, वे इस बात पर भी सहमत थे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास विशेष पद है और अन्य पदाधिकारियों की तुलना में उनके पास जो विचार हैं, वे लाभप्रद हैं।
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता की अवधारणा को शामिल करने का अर्थ होगा अनुच्छेद 217 के तहत प्रावधानों में एक प्रावधान को जोड़ना। इसका अंततः प्रावधान को फिर से लिखने का निहितार्थ होगा।
- उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रावधान की व्याख्या पदानुक्रमिक तरीके से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति को अपनी राय देने की दो मुख्य न्यायाधीशों की शक्ति कार्यात्मक है और पदानुक्रम के लिए अप्रासंगिक है। उन्होंने तर्क दिया कि महत्व कार्यात्मक प्रभावकारिता को दिया जाना चाहिए न कि प्राथमिकता के सवाल को।
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करते हैं और उनके प्रति जवाबदेह हैं। इसी तरह, न्यायपालिका को भी उसी तरह काम करना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार, न्यायिक नियुक्तियाँ कार्यपालिका द्वारा की जाती हैं क्योंकि यह संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह है।
न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता
- प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि न्यायाधीशों की संख्या के मुद्दे पर सवाल कायम नहीं रह गया है क्योंकि इसका निपटारा पहले ही सुभाष शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ (1990) के निर्णय में किया जा चुका है ।
- उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से वित्तीय निहितार्थ (इंप्लीकेश) भी होंगे, इसलिए इस संबंध में निर्णय लेने का काम संबंधित प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
- प्रतिवादियों ने अनुच्छेद 216 के तहत प्रावधान की तुलना अनुच्छेद 124 से की और बताया कि संसद बाद के प्रावधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय की संख्या निर्धारित करती है। तदनुसार, उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार संसद को छोड़ना चाहिए, न कि कार्यपालिका या न्यायपालिका को। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां यह महसूस किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की संख्या बढ़ाई जानी है, तो इसे कानून के माध्यम से संघ विधायिका द्वारा किया जाना चाहिए।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायालय संसद को कानून बनाने के लिए आदेश नहीं दे सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायालय को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला न्यायोचित नहीं है।
- इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का काम जानबूझकर राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है जो तकनीकी रूप से संसद या विधायिका के नियंत्रण में है जो न्यायाधीशों की संख्या की निरंतर समीक्षा या निर्धारण सुनिश्चित करेगी।
सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) में निर्णय
वर्तमान मामले में निर्णय 7:2 के अनुपात में सुनाया गया, जिसमें बहुमत की राय ने एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) के फैसले को खारिज कर दिया और संबंधित मुद्दों का सकारात्मक उत्तर दिया, जबकि अन्य दो न्यायाधीशों ने एक मुद्दे पर असहमति जताई।
न्यायालय ने प्राथमिकता के प्रश्न पर यह निष्कर्ष निकाला कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अद्वितीय (यूनिक), विलक्षण (सिंगुलर) और मौलिक (प्राइमल) है, लेकिन कार्यपालिका के साथ एकजुटता और पारस्परिकता के स्तर पर भागीदारीपूर्ण है, और न तो वह और न ही कार्यपालिका एक-दूसरे की इच्छा के विरुद्ध नियुक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं।
न्यायमूर्ति अहमदी और न्यायमूर्ति पुंछी द्वारा दिए गए अल्पमत निर्णय में कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई है, जबकि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के मामले में पुंछी ने कोई राय व्यक्त नहीं की, न्यायमूर्ति अहमदी ने न्यायमूर्ति वेंकटरमैया के साथ सहमति जताते हुए एस.पी. गुप्ता के मामले में इस मुद्दे पर सीमित अधिकार दिया।
बहुमत तथा असहमति जताने वाले न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय पर निम्नानुसार चर्चा की गई है।
नीचे चर्चित बहुमत का फैसला न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा और उनके चार सहयोगियों द्वारा दी गई राय के अनुसार है, न कि अन्य दो द्वारा जो अलग-अलग सहमति वाली राय हैं। फिर भी, इसमें बहुमत की राय में पहले से चर्चित पहलुओं के अलावा किसी भी अतिरिक्त पहलू पर दो सहमत न्यायाधीशों द्वारा दी गई टिप्पणियों या फैसलों पर भी चर्चा की गई है।
इसी तरह, नीचे चर्चा की गई असहमतिपूर्ण राय न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार है क्योंकि न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी न्यायमूर्ति अहमदी के समान ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, लेकिन उनके तर्क अलग थे। न्यायमूर्ति पुंछी ने यह भी कहा कि वे अपने सहयोगी से सहमत हैं, सिवाय उनके द्वारा बताए गए तर्क के।

बहुमत
इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों वाली पीठ के 7 न्यायाधीशों के बहुमत ने संबंधित मुद्दों का सकारात्मक उत्तर दिया। पांच न्यायाधीशों की बहुमत राय और दो सहमति वाली राय ने माना कि न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण से संबंधित मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता है। हालांकि, इसने माना कि उनकी प्रधानता एक संस्थागत निकाय के प्रमुख के रूप में है न कि एक व्यक्ति के रूप में। न्यायालय ने यह भी माना कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या पर निर्धारण का मामला एक हद तक न्यायोचित है।
न्यायालय ने बहुमत से फैसला सुनाया कि एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में ऊपर बताए गए मुद्दों के संबंध में बहुमत से दिया गया फैसला गलत है। तदनुसार, इसने फैसला सुनाया कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ संवैधानिक योजना की व्याख्या और क्रियान्वयन इस फैसले में निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए।
परामर्श का अर्थ
बहुमत ने फैसला सुनाया कि जब यह न्यायिक नियुक्तियों के उद्देश्य से भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित हो, तो ‘परामर्श’ शब्द का अर्थ या समझ, उस समझ और अर्थ से अलग होनी चाहिए जब यह उक्त उद्देश्य या प्रक्रिया में सहायता के लिए कार्यपालिका से संबंधित हो। उन्होंने देखा कि ‘सहमति’ के बजाय ‘परामर्श’ शब्द का उपयोग यह इंगित करने के लिए किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश सहित किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को कोई अत्यधिक विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई थी, भले ही उनकी राय का अधिक महत्व हो। यह एक प्रकार का नियंत्रण था जिसे कार्यपालिका द्वारा परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया था, जो मुख्य न्यायाधीश की शक्ति पर नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी है।
राय की प्रधानता
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत सभी न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता दी जाएगी और राष्ट्रपति द्वारा उनकी राय के उल्लंघन में कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए या कोई नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
बहुमत ने माना कि अनुच्छेद 74(1), 124(2) और 217(1) की व्याख्या सामंजस्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाद के दो प्रावधानों में निर्धारित संवैधानिक उद्देश्य पूरा हो। उन्होंने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिसे बदले में अनुच्छेद 124(2) और 217(1) की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना चाहिए।
उन्होंने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अंतिम राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, कार्यपालिका के साथ उम्मीदवार की अनुपयुक्तता के मजबूत कारणों की उपस्थिति में इसे नजरअंदाज किया जा सकता है और ऐसे कारणों को मुख्य न्यायाधीश को बताना होगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्राथमिकता एक संस्थागत प्रमुख के रूप में उनकी है, न कि किसी व्यक्ति की। यह एक सामूहिक राय है, जो उनके वरिष्ठ सहयोगियों के विचारों पर विचार करने के बाद बनाई गई है। उन्होंने कहा कि परामर्श प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश की राय न्यायपालिका की राय को प्रतिबिंबित करनी चाहिए।
उन्होंने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों पर विचार करने के बाद ही बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 124(2) के तहत कुछ अन्य न्यायाधीशों के विचारों पर विचार करना या उनका पता लगाना आवश्यक माना गया है। इसी तरह, उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के संबंध में, उन्होंने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों पर विचार करने या उनका पता लगाने के बाद ही अपनी राय बनानी चाहिए।
इसके अलावा, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही की जानी चाहिए। इसने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुसार किया गया स्थानांतरण न्यायोचित नहीं है।
इसने आगे यह भी निर्णय दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि इसके विपरीत कोई बाध्यकारी कारण मौजूद हो।
न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता
न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 216 राष्ट्रपति पर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का लगातार मूल्यांकन करने का दायित्व डालता है, जिसमें लंबित मामलों और भविष्य में दायर किए जाने की संभावना वाले मामलों को ध्यान में रखा जाता है। इसने माना कि अनुच्छेद 216 के तहत निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने में विफलता ऐसे दायित्व के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित होनी चाहिए। इसने फैसला सुनाया कि इस संबंध में अनुच्छेद 216 के तहत निर्धारित संवैधानिक दायित्व की समझ के संबंध में एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) के फैसले में बहुमत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत था।
हालांकि, इसने स्पष्ट किया कि मामले की न्यायसंगतता की सीमा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के अनुरूप प्रावधान के तहत उल्लिखित कर्तव्य को पूरा करने के निर्देश मात्र से आगे नहीं बढ़ती है। इसने फैसला सुनाया कि मामले की न्यायसंगतता का अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का आकलन करने और उसे स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है।
इसके अलावा, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, जिन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कि जब न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का कर्तव्य कार्यपालिका द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना हैं, तब उन्होंने फैसला सुनाया कि यदि किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की सिफारिश करता है और यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसी सिफारिश से सहमत होते हैं, तो कार्यपालिका के लिए अनुच्छेद 216 के तहत न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के अपने दायित्व को पूरा करना बाध्यकारी है।
मतभेद
बहुमत के फैसले पर न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी और न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी नामक दो न्यायाधीशों ने असहमति जताई। दोनों न्यायाधीशों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्राथमिकता के मुद्दे पर असहमति जताई। लेकिन दोनों, न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण के मुद्दे पर बहुमत से सहमत थे कि यह न्यायसंगत होना चाहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायसंगतता केवल सीमित सीमा तक और दुर्लभतम मामलों में ही होनी चाहिए।
परामर्श का अर्थ
न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा कि ‘परामर्श’ शब्द की सामान्य भाषा का तात्पर्य सलाह या विचार मांगना है और इसका अर्थ संवर्तन (कंकरेंस) या सहमति (कंसेंट) नहीं है। उन्होंने फैसला सुनाया कि इस शब्द का अर्थ यह नहीं है कि सलाह या विचार मांगने वाला व्यक्ति इसका पालन करने के लिए बाध्य है।
राय की प्रधानता
न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारों को संपूर्ण न्यायपालिका के सामूहिक या प्रतीकात्मक विचारों के रूप में मानना कठिन है, इसलिए राष्ट्रपति ऐसे विचारों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
उन्होंने फैसला सुनाया कि परामर्श की प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह को कार्यपालिका पर बाध्यकारी मानना अनुचित है। कार्यपालिका को ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने का मतलब होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को वीटो का अधिकार देना। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय देना समस्याग्रस्त है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचारों से बंधे हैं क्योंकि इससे संवैधानिक प्रावधानों और उनके उद्देश्यों में बदलाव या पुनर्लेखन होगा। परिणामस्वरूप, उन्होंने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क और विचार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस समय स्वीकार्य नहीं थे। इसलिए, उन्होंने निर्णय दिया कि उन्हें नहीं लगता कि एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में दिए गए निर्णय में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति पुंछी ने फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में कार्यपालिका के साथ भागीदारी की भूमिका है। उन्होंने कहा कि दोनों में से कोई भी दूसरे के विचारों के विरुद्ध नियुक्तियों के मामले में आगे नहीं बढ़ सकता।
न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता
जैसा कि ऊपर बताया गया है, न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी और न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी ने न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की न्यायसंगतता के मुद्दे पर बहुमत से सहमति जताते हुए फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अहमदी ने फैसला सुनाया कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना एक हद तक न्यायसंगत है और न्यायमूर्ति पुंछी ने कहा कि वे अपने सहयोगी से पूरी तरह सहमत हैं।
न्यायमूर्ति अहमदी ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का मुद्दा सीमित सीमा तक न्यायोचित है और इसे केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए। उन्होंने फैसला सुनाया कि यदि कार्यपालिका उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए बाध्य है और यदि वह इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है, तो न्यायालयों द्वारा कार्यपालिका को उचित समय के भीतर इस दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य करने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है।
अनुपात निर्णय
हालाँकि यह निर्णय 7:2 के अनुपात में दिया गया था, लेकिन माननीय न्यायाधीशों द्वारा अपनी-अपनी राय देने के लिए दिए गए तर्क अलग-अलग थे। पीठ द्वारा बताए गए प्रासंगिक कारणों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।
बहुमत
नीचे चर्चित अनुपात न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा और उनके चार सहयोगियों सहित पांच न्यायाधीशों की बहुमत राय द्वारा निर्धारित तर्क के अनुसार है।

न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा और चार अन्य
राय की प्रधानता
इस मामले में बहुमत के मत (जिसे आगे “न्यायालय” कहा जाएगा) ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय की प्रधानता के प्रश्न का निर्णय उसके पीछे के उद्देश्य या संवैधानिक योजना के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसने कहा कि यहाँ उल्लिखित उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करना है। इसलिए इसने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों की कोई भी व्याख्या जो उपर्युक्त उद्देश्य के विपरीत है, वह अवश्य ही अप्रिय होगी।
न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा किए गए इस दावे पर गौर किया कि न्यायिक नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामों की मंजूरी के बाद ही की गई हैं। न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा किया गया यह दावा कार्यपालिका द्वारा मुख्य न्यायाधीश को दी गई राय की प्राथमिकता को दर्शाता है।
न्यायालय ने कहा कि राय की प्रधानता तभी महत्वपूर्ण होती है जब सर्वसम्मति से निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए असहमति हो। इसलिए, प्रधानता उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो अपने उद्देश्य को संतोषजनक ढंग से प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी राय में सही होने की अधिक संभावना रखता हो। सरल शब्दों में, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उपर्युक्त संबंध में विशेषज्ञ माना जा सकता है।
न्यायालय ने कहा कि उच्चतर न्यायपालिका के लिए नियुक्तियाँ ऐसे व्यक्तियों की होती हैं जो या तो निचली अदालतों के न्यायाधीश होते हैं या बार के सदस्य होते हैं। दोनों ही मामलों में, ऐसे व्यक्तियों के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने का मुख्य स्थान न्यायालय ही होता है। इस प्रकार, उनकी विश्वसनीयता और महत्व का आकलन करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो संभवतः उम्मीदवारों के व्यक्तिगत गुणों को भी जानते होंगे क्योंकि उन्हें विभिन्न स्रोतों से ऐसी जानकारी मिलने की संभावना है। इसने बताया कि अपने-अपने न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श प्रक्रिया की शुरूआत इस अहसास के साथ की गई थी कि मुख्य न्यायाधीश उच्चतर न्यायपालिका के लिए नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवार की योग्यता और विश्वसनीयता को जानने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित होंगे। इसने यह भी कहा कि इस तरह की शुरूआत के पीछे का उद्देश्य न्यायिक नियुक्तियों पर राजनीतिक प्रभाव को रोकना था।
न्यायालय ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में वास्तविक जवाबदेही भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की है, क्योंकि वे न्यायालयों के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं और यदि कोई अनुपयुक्त नियुक्ति की गई तो उन्हें परिणाम और आलोचना का सामना करना पड़ेगा।
न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हुए एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा की गई टिप्पणी पर गौर किया, जिसमें उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत के रूप में कानून के शासन पर गौर किया था, जिसे प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तदनुसार, उन्होंने देखा कि कानून के शासन में गैर-मनमानी शामिल है, जिसे न्यूनतम विवेक और विभिन्न विचारों पर विचार करके सामूहिक निर्णय लेने से प्राप्त किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि निर्णय लेते समय वैध अपेक्षाओं पर विचार करना भी गैर-मनमानी के नियम का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसलिए न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी इसका पालन करना चाहिए।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति के अनुसार नियुक्ति करने से उन असाधारण मामलों में मना कर सकते हैं, जहां राष्ट्रपति के कार्य को उचित ठहराने के लिए बाध्यकारी कारण हों। इसने कहा कि कई बार मुख्य न्यायाधीश के अलावा कुछ अन्य पदाधिकारी भी हो सकते हैं, जो अनुशंसित उम्मीदवार की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि आदि जैसी जानकारी जानने की बेहतर स्थिति में होंगे। इसने आगे कहा कि ऐसी सामग्री या जानकारी मुख्य न्यायाधीश को अवश्य बताई जानी चाहिए।
न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता
इस मामले में बहुमत के मत से यह माना गया कि अनुच्छेद 216 के तहत दायित्व का अधिरोपण शीघ्र सुनवाई और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, जो राष्ट्र के शासन में एक महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत भी है। इसने कहा कि इस तरह के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करना और संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है।
न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायालय की मौजूदा संख्या लोगों को त्वरित न्याय और त्वरित सुनवाई प्रदान करने के लिए अपर्याप्त लगती है, जो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का एक पहलू है, तो अपर्याप्तता का आकलन करने और तदनुसार संख्या निर्धारित करने के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के आकलन और निर्धारण से न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी प्रणाली को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है।
न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 216 के तहत प्रावधान की अलग से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। इसके बजाय, इसे अंतिम संवैधानिक योजना के एक भाग के रूप में समझा जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि प्रावधान की ऐसी व्याख्या इसमें निर्धारित दायित्व या कर्तव्य को एक निश्चित सीमा तक न्यायोचित बनाएगी।
मतभेद
नीचे चर्चा की गई असहमतिपूर्ण राय का औचित्य न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी द्वारा दिए गए विचारों के अनुसार है। न्यायमूर्ति एम.एम. पुंची ने कहा कि वे अपने असहमत सहयोगी की राय से सहमत हैं।
न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी
राय की प्रधानता
माननीय न्यायमूर्ति अहमदी ने याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार किया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि “केंद्र सरकार ने वास्तविक व्यवहार में हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति को प्राथमिकता दी है और उनकी राय के विपरीत की गई नियुक्तियाँ बहुत कम हैं, इसलिए, एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए” क्योंकि यह अस्थिर है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों से संबंधित मामलों में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि आम सहमति पर पहुँचने के लिए मिलकर काम करते हैं। इसलिए, आम सहमति पर पहुँचने के बाद मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप नियुक्तियाँ करना संभव है और यह निर्णय पर पुनर्विचार का औचित्य नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अनुच्छेद 217(1) के तहत उल्लिखित तीन संवैधानिक पदाधिकारियों से परामर्श एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि नियुक्ति की अंतिम शक्ति राष्ट्रपति के पास है, जिन्हें अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।
उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता के तीन मुख्य पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया।
- भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में मुख्य न्यायाधीश की प्रधानता।
- अनुच्छेद 124(2) और 217(1) के तहत सभी परामर्शदाताओं के बीच उनके विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- उनकी राय या विचारों की प्रधानता जो राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका पर बाध्यकारी है।
न्यायमूर्ति अहमदी ने पहले पहलू के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश की विशिष्ट स्थिति, उस पद में निहित अधिकार और शक्तियों तथा उनके द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों का उल्लेख किया। तदनुसार, उन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस सीमित सीमा तक ही प्राथमिकता प्राप्त है।
न्यायमूर्ति अहमदी ने दूसरे पहलू की जांच करते हुए पाया कि अनुच्छेद 124(2) और विशेष रूप से अनुच्छेद 217(1) के तहत प्रावधान में वर्णित परामर्शदाताओं (संवैधानिक पदाधिकारियों) के बीच किसी भी प्रकार का पदानुक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा दी गई किसी भी राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य परामर्शदाताओं द्वारा दी गई राय को अवांछित मानना अनुचित है, यदि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि सलाह को अधिक महत्व देना उसे अंतिम मानने से अलग है। जबकि पहला वाला उचित और संभव है, दूसरा वाला अन्य परामर्शदाताओं के लिए अनुचित है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार, मुख्य न्यायाधीश के विचारों को उन पर बाध्यकारी बनाने का अर्थ यह होगा कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ऐसे विचारों से बंधी हुई है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह की व्याख्या का मतलब संविधान को फिर से लिखना और संविधान द्वारा निर्धारित भूमिकाओं, पदों और संरचनाओं को बदलना होगा। इसलिए, उन्होंने कहा कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है।
अंततः, तीसरे पहलू के संबंध में, उन्होंने कहा कि ‘परामर्श’ शब्द का सीधा अर्थ सलाह और राय लेना है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि परामर्श मांगने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसी सलाह या राय का पालन करने के लिए बाध्य है।
हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी प्रावधान की व्यापक व्याख्या करना या समाज में होने वाले बदलावों के अनुसार उसे ढालना उचित हो सकता है, लेकिन व्यापक व्याख्या की आड़ में प्रावधानों को फिर से लिखना या बदलना अस्वीकार्य है। तदनुसार, उन्होंने कहा कि यह इंगित करना संभव नहीं है कि ‘परामर्श’ शब्द का अर्थ सहमति या संवर्तन है।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 320 (3) और 323 के तहत प्रावधानों का उल्लेख किया जो लोक सेवा आयोग के परामर्श के लिए प्रदान करते हैं। यदि सरकार आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं करती है तो इन प्रावधानों में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी प्रावधान है। इसलिए, न्यायमूर्ति अहमदी ने कहा कि संविधान स्वयं ही परामर्शदाता द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार न करने की संभावना को निर्धारित करता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनबोधन लाल श्रीवास्तव (1957) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया हैं जिसमें न्यायालय ने कहा कि “परामर्श की आवश्यकता आयोग द्वारा दी गई सलाह को सरकार के लिए बाध्यकारी बनाने के लिए नहीं है।” तदनुसार, उन्होंने कहा कि कार्यपालिका पर बाध्यकारी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह पर विचार करने से मुख्य न्यायाधीश को वीटो का अधिकार मिलेगा जो मौजूदा संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है।

न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता
न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति अहमदी ने इस संबंध में एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में न्यायमूर्ति तुलजापुकर के दृष्टिकोण को नोट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ” न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को रिट या निर्देश जारी करे जब तक कि स्पष्ट परिस्थितियों द्वारा मजबूर न किया जाए क्योंकि यह पूरी तरह से कार्यकारी कार्य है।” उन्होंने न्यायमूर्ति वेंकटरमैया के दृष्टिकोण पर भी गौर किया जिसमें उन्होंने फैसला दिया था कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के मुद्दे को एक सीमित सीमा तक न्यायिक समीक्षा के अधीन किया जा सकता है जैसे कि अनुच्छेद 216 के तहत कर्तव्य के पालन के लिए मात्र निर्देश जारी करना। तदनुसार, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की समीक्षा करने और उसे निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को रिट या निर्देश जारी करने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा सीमित सीमा तक और असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है।
उन्होंने न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण की न्यायसंगतता के मुद्दे को तय करने के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच की। उन्होंने कहा कि कर्तव्य के प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा 3 आधारों पर की जा सकती है, अर्थात् अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनुचितता। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में जहां कर्तव्य विवेकाधीन नहीं है, लेकिन कानून के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जाना है और यदि इसे नहीं किया गया है, तो न्यायालय ऐसे कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए परमादेश जारी कर सकते हैं।
इसके अलावा, न्यायमूर्ति अहमदी ने विवेकाधीन प्रकृति के कर्तव्यों से संबंधित न्यायिक समीक्षा के दायरे की जांच की। उन्होंने कहा कि कार्यकारी प्राधिकरण को अपने विवेक का प्रयोग करने और यह तय करने के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है कि क्या इस तरह के विवेकाधीन कर्तव्य का प्रदर्शन न्यायसंगत समय के भीतर आवश्यक है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के सीमित प्रकृति के परमादेश को केवल ठोस कानूनी सिद्धांतों के समर्थन के साथ ही जारी किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने फैसला सुनाया कि न्यायाधीशों की संख्या तय करने के लिए सीमित प्रकृति का परमादेश या निर्देश भी जारी किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) का विश्लेषण
न्यायालय ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय हुई विभिन्न बहसों और स्वतंत्रता-पूर्व युग के विधानों में न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित प्रावधानों पर भी गौर किया। उन्होंने कहा कि संबंधित प्रावधानों में परामर्श प्रक्रिया को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य न केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद बल्कि उनकी नियुक्ति के दौरान भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। यह सुनिश्चित करना था कि न्यायिक नियुक्तियाँ किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हों।
न्यायालय ने इस मामले में शामिल प्रमुख संवैधानिक मुद्दों की जांच के लिए विभिन्न मिसालों, अन्य देशों में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण न्यायिक कार्यों का भी हवाला दिया और अंततः न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए एक संतुलित निर्णय दिया। हालाँकि यह निर्णय सही नहीं रहा होगा, लेकिन इसने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यकारी प्रभाव से मुक्त हो, क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण का एक निहित पहलू है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 50 में भी किया गया है।
इसके साथ ही, यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में न्यायालय कॉलेजियम प्रणाली से जुड़ी कुछ अन्य प्रासंगिक चिंताओं, जैसे पारदर्शिता या जवाबदेही की कमी, का समाधान करने में विफल रहा।
मुद्दावार विश्लेषण
निर्णय का मुद्दावार विश्लेषण इस प्रकार है।
‘परामर्श’ शब्द का अर्थ
पहला बड़ा मुद्दा अनुच्छेद 124 में आने वाले “परामर्श” शब्द का अर्थ था। बहुमत ने माना कि यह एक एकीकृत, सहभागी और परामर्शी प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों की ओर से संवैधानिक दायित्वों का पूर्ण निर्वहन शामिल है। न्यायाधीशों द्वारा यह दिखाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है कि “परामर्श” का अर्थ घटना या प्रधानता है, जिनमें से विशेष रूप से निम्मलिखित दृष्टिकोण हैं”
भारत के मुख्य न्यायाधीश एक ‘ पैटरफैमिलियास ‘ (परिवार के मुखिया) के रूप में निर्णय देने की सर्वोत्तम स्थिति में होंगे।
अन्य संविधानों के विपरीत, भारतीय संविधान में कार्यपालिका के हाथों में पूर्ण विवेकाधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को निम्न पद नहीं माना जा सकता।
नियुक्तियों की प्रथा संविधान का अभिन्न अंग बन गई है, जिसके कारण एक परंपरा का निर्माण हुआ है। यह परंपरा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नियुक्ति करने की अनुमति नहीं देती है।
चूंकि केन्द्र सरकार न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामलों में वादी है, इसलिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति में पक्ष नहीं हो सकती।
सभी न्यायाधीशों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने को भी इसका कारण बताया है।
प्रस्ताव की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के मामले में, प्रस्ताव उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आना चाहिए। उम्मीद की जाती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश स्थानांतरण के लिए कोई भी प्रस्ताव शुरू करेंगे। इसके अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर एक चेक रखा गया है, जो अब अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के साथ परामर्श करने के लिए बाध्य हैं। इस प्रकार भारत के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। यदि कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दो संभावनाएँ हैं। ये सबसे वरिष्ठ सहयोगियों की सहमति पर निर्भर करते हैं। अन्य दो न्यायाधीशों का विचार है कि इसे वापस लिया जाना चाहिए, सिफारिश को वापस ले लिया जाएगा। हालाँकि, यदि वे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सहमति में हैं, तो सिफारिश फिर से की जाएगी और इसे स्वीकार करना होगा।

नियुक्ति के लिए मानदंड
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में, बहुमत ने माना कि वरिष्ठता ही प्रचलित मानदंड होना चाहिए, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति योग्य हो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वरिष्ठता के साथ-साथ उनकी संयुक्त वरिष्ठता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यायाधीशों की वैध अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण
स्थानांतरित व्यक्ति की सहमति अप्रासंगिक है। हालांकि, स्थानांतरण करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को स्थानांतरित व्यक्ति के व्यक्तिगत कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। यह एस.पी गुप्ता मामले में दिए गए निर्णय के अनुरूप है। प्रभावित स्थानांतरणों को दंडात्मक नहीं माना जाना चाहिए।
ऐसे स्थानांतरणों की न्यायसंगतता संभव नहीं है, सिवाय इस आधार पर कि स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों पर नहीं किया गया था।
न्यायाधीश की शक्ति की न्यायसंगतता
न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण न्यायोचित है, लेकिन यह दिखाया जाना चाहिए कि शक्ति की कमी “न्याय में देरी” की ओर ले जाती है, (जैसा कि यह अनुच्छेद 21 द्वारा अनिवार्य है कि आपराधिक मुकदमों के संबंध में न्यायालयों में त्वरित न्याय एक मौलिक अधिकार है) भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की नियुक्ति
न्यायमूर्ति रत्नावेल पांडियन ने अपने फैसले का एक बड़ा हिस्सा कुछ वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालने में लगाया है। उन्होंने यह दिखाने के लिए आंकड़े पेश किए हैं कि महिलाओं, ओबीसी, एससी और एसटी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसलिए, उन्होंने सरकार पर इन वर्गों की सूची आगे बढ़ाने का दायित्व डाला है, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश निर्णय लेंगे।
संदर्भित उदाहरण
पीठ ने मामले में शामिल मुद्दों की जांच करते समय विभिन्न मिसालों को देखा और उनका संदर्भ दिया। जिस मौलिक निर्णय का संदर्भ दिया गया वह एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) था क्योंकि यह वह निर्णय था जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा था। कानून के शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों के स्थानांतरण और कई अन्य पहलुओं से संबंधित कई प्रासंगिक टिप्पणियों को तत्काल मामले में पीठ द्वारा नोट किया गया, पुष्टि की गई और असहमत किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो नोट किया गया वह सुभाष शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ (1990) था क्योंकि यह भी उसी संबंध में था।
पीठ ने मुद्दों का विश्लेषण करते समय कई अन्य प्रासंगिक उदाहरणों को भी नोट किया और उनका संदर्भ दिया। बहुमत की राय में नोट किए गए कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।
न्यायिक जवाबदेही पर उप-समिति बनाम भारत संघ (1991)
न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की जांच करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक जवाबदेही उप-समिति बनाम भारत संघ (1991) के मामले में संविधान पीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर गौर किया।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 के तहत न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित मुद्दों पर दायर रिट याचिकाओं पर विचार कर रहे थे। न्यायालय ने नोट किया था कि यह मामला अनुच्छेद 121 और 124 की व्याख्या और न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 से संबंधित संवैधानिक महत्व के मुद्दों से जुड़ा था।
उक्त मामले में पीठ ने टिप्पणी की थी कि न्यायालयों के लिए मामले की योग्यता की जांच करने से पहले न्यायपालिका और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का सारांश लेना आवश्यक है। इसने फैसला सुनाया था कि न्यायालय को ऐसे प्रावधानों की व्याख्या करते समय ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो संविधान की मौलिक विशेषताओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करे। यह देखा गया कि कानून का शासन संविधान की एक मौलिक विशेषता है जो संवैधानिक ढांचे में सन्निहित है। इसके अलावा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कानून के शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना गया।
माननीय न्यायालय ने उपर्युक्त टिप्पणियों पर गौर करते हुए कहा कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या संवैधानिक ढांचे की मौलिक अवधारणाओं के अनुरूप होनी चाहिए।
इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975)
न्यायालय ने कानून के शासन की अवधारणा और सार्वजनिक अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे पर चर्चा करते हुए इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) में अवधारणा के महत्व के बारे में माननीय न्यायमूर्ति मैथ्यू द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ चुनौती पर विचार कर रहा था जिसमें न्यायालय ने चुनावी कदाचार के आधार पर अपीलकर्ता की सीट खाली कर दी थी।
इस मामले में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें बहुमत के मत से यह निर्णय लिया गया था कि कानून का शासन लोकतंत्र के साथ-साथ संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कानून का शासन कानून की भावना की सार्वभौमिकता को दर्शाता है, जो सरकारी अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई को बाहर करता है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की अवधारणा किसी अव्यक्त चीज को वास्तविकता में बदलना है। उन्होंने आगे कहा कि कानून के शासन की अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है और इसका उद्देश्य कानून के दो विपरीत पहलुओं यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है। उन्होंने सर आइवर जेनिंग्स की राय का भी उल्लेख किया, जहां उन्होंने इस अवधारणा को एक अनियंत्रित घोड़ा कहा था।

न्यायमूर्ति मैथ्यू ने आगे इस अवधारणा की डाइसी की परिभाषा पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने इसे ” नियमित कानून की पूर्ण सर्वोच्चता या प्रबलता, मनमाने अधिकार के प्रभाव के विपरीत, सरकार की ओर से मनमानी, विशेषाधिकार, यहां तक कि व्यापक विवेकाधीन अधिकार के अस्तित्व को छोड़कर” के रूप में समझाया है।
तदनुसार, उपर्युक्त टिप्पणियों पर गौर करने के बाद, न्यायालय ने (बहुमत की राय से) तत्काल मामले में फैसला सुनाया कि कानून के शासन के कामकाज के भीतर विवेकाधीन शक्ति के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, भले ही ऐसी विवेकाधीन शक्ति न्यूनतम हो।
अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य (1985)
वर्तमान मामले में न्यायालय ने अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य (1985) में न्यायिक नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित मामले में माननीय न्यायमूर्ति भगवती द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस निर्णय के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (अपील) पर विचार कर रहा था, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा एवं अन्य संबंधित सेवाओं में किए गए कुछ चयनों को रद्द कर दिया गया था। इस मामले में संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति भगवती ने न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया पर चर्चा और जांच करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को आमंत्रित करने की प्रथा पर गौर किया। उन्होंने कहा कि राज्य न्यायिक सेवाओं के लिए नियुक्तियां करते समय यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि इस पद के लिए योग्य और निष्ठावान व्यक्तियों का चयन किया जाए। उन्होंने आगाह किया कि इस तरह की सावधानी न बरतने पर अयोग्य और बेईमान न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है जो राज्य की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरा पैदा करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बजाय विशेष रूप से साक्षात्कार में उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को नामित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नामांकन इस तथ्य के कारण है कि वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में ऐसा नामित व्यक्ति साक्षात्कार के लिए आने वाले उम्मीदवारों की गुणवत्ता और निष्ठा को जानता है।
इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि मनोनीत व्यक्ति द्वारा दी गई सलाह को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी सलाह को स्वीकार नहीं किया जा सकता, बशर्ते कि अस्वीकृति के लिए मजबूत कारण मौजूद हों, जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
वर्तमान मामले में न्यायालय (बहुमत की राय) ने उपर्युक्त टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की तथा निर्णय दिया कि यह उच्च न्यायपालिका में की गई नियुक्तियों पर भी लागू होता है।
भारत संघ बनाम संकल चंद हिम्मतलाल शेठ (1977)
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण करने के लिए पूर्व सहमति के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए भारत संघ बनाम संकल्प चंद हिम्मतलाल शेठ (1977) में दिए गए फैसले पर गौर किया।
इस मामले में न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज करने के निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर विचार कर रहा था। अपीलकर्ता, जो एक न्यायाधीश था, ने उक्त रिट याचिका के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें अपीलकर्ता को गुजरात उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रावधान था। उन्होंने इस आधार पर स्थानांतरण को चुनौती दी थी कि स्थानांतरण उनकी पूर्व सहमति के बिना प्रस्तावित किया गया था, जिसे अनुच्छेद 222 के अनुसार अपेक्षित माना गया था। विशेष तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्थानांतरण की अधिसूचना के खिलाफ अपीलकर्ता की चुनौती को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था।
इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और उसके बाद स्थानांतरण की अधिसूचना को बरकरार रखा। इसने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 222 के तहत प्रावधान की व्याख्या द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि किसी न्यायाधीश को उसकी पूर्व सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता हैं। इसने माना कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की शक्ति संविधान द्वारा जनहित में राष्ट्रपति को प्रदान की गई है और इस शक्ति का प्रयोग केवल जनहित में ही किया जा सकता है।
न्यायालय ने इस मामले में उपर्युक्त टिप्पणियों और फैसले की पुष्टि की और माना कि अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण से पहले न्यायाधीश की पूर्व सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसने माना कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण का पूरा मुद्दा पहले ही ऊपर उल्लिखित मामले में और एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में तय किया जा चुका है और इसलिए इसे दोहराना आवश्यक नहीं है।
ऊपर चर्चित मामलों के अतिरिक्त, अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे के.एम नानावटी बनाम बॉम्बे राज्य (1960) , ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) , बंगाल इम्युनिटी बनाम बिहार राज्य (1955) , शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) , इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) , आर.सी पौडयाल बनाम भारत संघ (1993) आदि को भी अन्य सहमत और असहमत न्यायाधीशों द्वारा अंकित किया गया और संदर्भित किया गया।
फैसले के बाद की स्थिति
इस निर्णय के बाद से न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कई घटनाक्रम देखने को मिले हैं। इस निर्णय के तत्काल परिणामों में से एक कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना थी, जिसके बाद तीसरे न्यायाधीशों के मामले में इसे मजबूत किया गया। तीसरे न्यायाधीशों के मामले के लगभग दो दशक बाद, कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए कानून बनाया गया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चौथे न्यायाधीशों के मामले में खारिज कर दिया था, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को बरकरार रखा गया था। वर्तमान में, न्यायिक नियुक्तियाँ कॉलेजियम प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं।
कॉलेजियम प्रणाली
कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या संरचना को संदर्भित करती है। यह कॉलेजियम द्वारा न्यायिक नियुक्तियों की एक प्रक्रिया या तंत्र है। यह विशेष प्रणाली न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से विकसित हुई है और इसे तत्काल मामले में निर्धारित किया गया था।
इस प्रणाली के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रीय स्तर पर तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में राज्य स्तर पर एक कॉलेजियम मौजूद होता है।
कॉलेजियम तीन सदस्यीय निकाय को संदर्भित करता है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के उनके दो वरिष्ठतम सहकर्मी शामिल होते हैं। किसी उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ उनके दो वरिष्ठतम सहकर्मी शामिल होते हैं।

कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं जो इस प्रकार हैं।
- किसी न्यायाधीश की नियुक्ति या स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम द्वारा नामों की सिफारिश।
- कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार न्यायाधीश(यों) की नियुक्ति या स्थानांतरण।
तीसरे न्यायाधीश का मामला
विशेष संदर्भ संख्या 1, 1998 का मामला , जिसे तीसरे न्यायाधीश का मामला भी कहा जाता है, किसी प्रकार की याचिका या जनहित याचिका नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजा गया एक संदर्भ है।
भारत के राष्ट्रपति ने 23 जुलाई, 1998 को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित कानून के प्रश्नों पर विचार करने और तदनुसार अपने विचार/राय प्रस्तुत करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेष संदर्भ दिया। राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट मुद्दों पर एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में व्यापक रूप से निर्णय लिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानून के प्रश्नों/मुद्दों की जांच की और 28 अक्टूबर 1998 को अपना निर्णय सुनाया और एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) में दिए गए अपने निर्णय की पुष्टि की।
राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ भेजे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह था कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(2) के तहत केवल दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए या व्यापक परामर्श की आवश्यकता है।
इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को मजबूत किया। न्यायालय ने कॉलेजियम की संरचना को तीन सदस्यीय निकाय से बढ़ाकर पांच सदस्यीय निकाय कर दिया। इसने मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठतम सहयोगियों की संरचना को बदलकर चार वरिष्ठतम सहयोगियों की संरचना कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की संरचना वही रही।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) और चौथा न्यायाधीश मामला
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (जिसे आगे “आयोग” या “एनजेएसी” कहा जाएगा) एक निकाय था जिसकी स्थापना न्यायिक नियुक्तियाँ करने के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए की गई थी। इस आयोग की स्थापना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 के तहत की गई थी, जिसे 2014 में न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करने के लिए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के साथ लागू किया गया था ।
99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 124A , 124B और 124C जोड़े गए , जो आयोग की स्थापना, संरचना और कार्यों के लिए प्रावधान करते हैं। आयोग की संरचना में निम्नलिखित शामिल थे।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे
- सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री।
- दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सभा में विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा नामित किया जाएगा।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ (2015) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को इस मामले में अपना निर्णय सुनाया और दोनों विवादित विधानों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया तथा न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022
कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के हालिया प्रयासों में, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक, 2022 , संविधान संशोधन विधेयक, 2022 के साथ 2022 में राज्यसभा में पेश किया गया था।
विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 124A से 124E को शामिल करके न्यायिक नियुक्तियां करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के समान ही था, सिवाय इसके कि इसकी संरचना में एक बदलाव किया गया था। नवीनतम विधेयक में, केंद्रीय विधि मंत्री के स्थान पर भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया गया। यद्यपि यह विधेयक राज्य सभा में पारित हो गया था, लेकिन बाद में इस संबंध में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई।
वर्तमान पद
वर्तमान में न्यायिक नियुक्तियाँ कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती हैं। हालाँकि इस प्रणाली को हाल के दिनों में विभिन्न आलोचनाओं और कुछ अनुचित देरी का सामना करना पड़ा है, फिर भी इसे बरकरार रखा गया है।
कॉलेजियम की संरचना वर्तमान में तीसरे न्यायाधीश के मामले में दिए गए निर्णय पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम पांच सदस्यीय निकाय है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके चार वरिष्ठतम सहकर्मी शामिल होते हैं, जबकि उच्च न्यायालय का कॉलेजियम तीन सदस्यीय निकाय है जिसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके दो वरिष्ठतम सहकर्मी शामिल होते हैं।
आलोचनाएं
कॉलेजियम प्रणाली की विभिन्न उदाहरणों में बार के सदस्यों, नागरिक समाज, सरकार और कभी-कभी पूर्व न्यायाधीशों द्वारा भी पारदर्शिता, जवाबदेही और हाल ही में कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी जैसे विभिन्न आधारों पर कड़ी आलोचना की गई है। हालांकि, बार के सदस्यों के साथ-साथ न्यायपालिका द्वारा भी इस प्रणाली की आलोचना की गई है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इस समय कॉलेजियम प्रणाली ही एकमात्र बेहतर विकल्प है।
आलोचना का एक प्रमुख आधार पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। कॉलेजियम प्रणाली की अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होने वाली प्रक्रिया के रूप में आलोचना की जाती है। कॉलेजियम की प्रक्रिया और कामकाज को अक्सर सार्वजनिक स्थान के सामने नहीं रखा जाता है, जो प्रणाली में पारदर्शिता के बारे में चिंताएँ पैदा करता है। कॉलेजियम की जवाबदेही की कमी के कारण भी इसकी आलोचना की जाती है। कॉलेजियम पूरी तरह से कार्यपालिका से अलग है और किसी भी प्रशासनिक निकाय के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप जाँच और संतुलन या जवाबदेही की प्रणाली का अभाव है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कि यह प्रणाली का कामकाज होता है और इसे जनता के सामने नहीं रखा जाता है, जो इसे सीधे जनता के प्रति भी जवाबदेह नहीं बनाता है।
न्यायिक नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद और पक्षपात की संभावनाओं से संबंधित चिंताओं के कारण भी कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की जाती है। साथ ही, असमान प्रतिनिधित्व भी जनता के बीच चिंता का विषय है, जिससे इस प्रणाली की आलोचना होती है।
इसके अतिरिक्त, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में हाल ही में विकसित हुई प्रमुख चिंताओं में से एक कॉलेजियम और कार्यपालिका के बीच नियुक्ति की सिफारिश और स्थगन का दुष्चक्र है। हाल के दिनों में यह देखा गया है कि नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा कार्यपालिका को अनुशंसित कुछ नामों को या तो लंबे समय तक विलंबित किया जाता है या ऐसी कार्रवाई के लिए कोई कारण बताए बिना नियुक्ति के बिना ही वापस कर दिया जाता है। इससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक तरह की खींचतान पैदा हो गई है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बनाए रखते हुए प्रणाली से जुड़ी चिंताओं को दूर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूचना के अधिकार के दायरे में प्रक्रिया को शामिल करना एक समाधान हो सकता है। चूंकि न्यायिक नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति को नामित करते समय न्यायाधीशों के विचार पहले से ही लिखित रूप में दर्ज होते हैं, इसलिए चिंताओं को दूर करने के लिए उन्हें सार्वजनिक कार्यक्षेत्र (डोमेन) में रखना उचित होगा। इससे जवाबदेही के पहलू को संबोधित करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि पारदर्शिता और जवाबदेही एक साथ चलते हैं।

निष्कर्ष
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को छुआ और उस पर फैसला सुनाया तथा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जो उस समय उचित हो सकता था। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बदलते परिदृश्यों के अनुसार बदलाव आवश्यक हैं। यद्यपि माननीय न्यायालय ने तीसरे न्यायाधीशों के मामले में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया, फिर भी कुछ खामियां या चिंताएं थीं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता थी और जो आज भी मौजूद हैं।
नागरिकों के सूचना के अधिकार अधिनियम को सुरक्षित करने के लिए कानून का अधिनियमन, जो नागरिकों को सार्वजनिक मामलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और अंततः उन्हें जवाबदेही मांगने का अधिकार देता है, सार्वजनिक मामलों से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। जबकि न्यायालयों ने हमेशा लगभग सभी सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता के कारण को आगे बढ़ाया है, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, भले ही यह गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए न्यूनतम सीमा तक हो। पारदर्शिता और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना और उसे सभी प्रकार के कार्यकारी प्रभाव से बचाना आवश्यक है, जो कॉलेजियम प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि, प्रक्रिया के बारे में चिंताओं को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे न्यायिक नियुक्तियों और अन्य न्यायिक मामलों में जनता का विश्वास मजबूत होगा, जो वर्तमान में कुछ हद तक कम होता दिख रहा है। ऊपर बताए गए सुझावों में से किसी एक को लागू करके या उसका प्रयोग करके न्यायपालिका की पारदर्शिता और स्वतंत्रता का संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
किस मामले को “प्रथम न्यायाधीश मामला” कहा जाता है?
एस.पी गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) को प्रथम न्यायाधीश मामले के रूप में जाना जाता है।
‘प्रथम न्यायाधीश मामले’ में क्या निर्णय दिया गया?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) मामले में माना कि न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसने यह भी माना कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के मामले को न्यायिक समीक्षा या कार्यपालिका को आदेश जारी करके तय नहीं किया जा सकता।
किस मामले को “द्वितीय न्यायाधीश मामला” कहा जाता है?
वर्तमान मामला, सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ (1993) को लोकप्रिय रूप से द्वितीय न्यायाधीश मामला के रूप में जाना जाता है।
“द्वितीय न्यायाधीश मामले” में क्या निर्णय दिया गया?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ (1993) में प्रथम न्यायाधीश मामले में स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया।
इसने फैसला सुनाया कि न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्राथमिकता दी जाती है। इसने यह भी फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का मामला एक हद तक न्यायोचित है।
किस मामले को “तृतीय न्यायाधीश मामले” कहा जाता है?
विशेष संदर्भ संख्या 1, 1998 को लोकप्रिय रूप से तृतीय न्यायाधीश मामले के रूप में जाना जाता है।
यह मामला संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा द्वितीय न्यायाधीश मामले में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया एक विशेष संदर्भ है।
“तृतीय न्यायाधीश मामले” में क्या निर्णय दिया गया?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ (1993) के फैसले की पुष्टि की तथा कॉलेजियम प्रणाली द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को मजबूत किया।
इसने कॉलेजियम की संरचना को 3 सदस्यीय निकाय से बढ़ाकर 5 सदस्यीय निकाय कर दिया।
किस मामले को “चौथे न्यायाधीश का मामला” कहा जाता है?
सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एवं अन्य बनाम भारत संघ (2015) को चौथे न्यायाधीश मामले के रूप में जाना जाता है।
“चौथे न्यायाधीश मामले” में क्या निर्णय दिया गया?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को असंवैधानिक घोषित किया तथा न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा।
उपर्युक्त विधानों में कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर न्यायिक नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
किस मामले के परिणामस्वरूप कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई?
दूसरे न्यायाधीश मामले यानी सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (1993) के मामले ने कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की। इसके अलावा, तीसरे न्यायाधीश मामले ने कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया को मजबूत किया।
न्यायिक नियुक्तियों की वर्तमान प्रक्रिया क्या है?
वर्तमान में न्यायिक नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं।
कॉलेजियम प्रणाली क्या है?
कॉलेजियम प्रणाली कॉलेजियम द्वारा न्यायिक नियुक्तियों की एक प्रक्रिया या तंत्र है। यह प्रणाली न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
इस प्रणाली में दो चरण होते हैं, अर्थात् कॉलेजियम द्वारा नियुक्तियों और स्थानांतरण के लिए नामों की सिफारिश और उसके बाद सरकार द्वारा नियुक्ति।
कॉलेजियम वर्तमान न्यायाधीशों के एक समूह को संदर्भित करता है जो न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों के लिए नामों पर निर्णय लेता है और उनकी सिफारिश करता है।
कॉलेजियम की संरचना क्या है?
सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम पांच न्यायाधीशों से बना होता है, जिसमें कॉलेजियम के प्रमुख के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उनके चार अन्य वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं।
उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उस न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन या नियुक्ति कैसे होती है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की तिथि से तय होती है।
संदर्भ
- https://blog.ipleaders.in/an-overview-of-njac-vis-a-vis-collegium-system-w-r-t-the-indian-judiciary/