यह लेख Almana Singh द्वारा लिखा गया है। यह राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेंदोलकर के मामले में दिए गए निर्णय का विस्तृत विश्लेषण करता है, जिसमें तथ्यों, उठाए गए मुद्दों, दिए गए तर्कों के साथ-साथ जांच आयोग अधिनियम, 1952 और भारत के संविधान के संबंधित कानूनी प्रावधानों का भी उल्लेख है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
यह लेख श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेंदोलकर और अन्य (1958) के मामले में उठाए गए मुद्दों, दिए गए तर्कों और सुनाए गए निर्णय से संबंधित है। इस मामले में, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (जिसे यहां “अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया गया है) की संवैधानिकता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई थीं। यह तर्क दिया गया था कि यह अधिनियम सरकार को “सार्वजनिक महत्व” के मामलों को संबोधित करने की आड़ में निजी व्यक्तियों और कंपनियों के मामलों की जांच करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जो संभावित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इन तर्कों के बावजूद, न्यायालय ने अधिनियम और 11 दिसंबर 1956 की अधिसूचना दोनों की वैधता को बरकरार रखा।
मामले का विवरण
- मामले का नाम– श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर एवं अन्य।
- याचिकाकर्ता– श्री राम कृष्ण डालमिया
- प्रतिवादी– श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर
- न्यायालय– भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- मामले का प्रकार– सिविल अपील संख्या 455 से 457 और 656 से 658, 1957
- निर्णय की तिथि– 28.03.1958
- न्यायपीठ– भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुधी रंजन दास, न्यायमूर्ति ए.के. सरकार, न्यायमूर्ति बी.पी. सिन्हा, न्यायमूर्ति एस.के. दास और न्यायमूर्ति टी.एल. वेंकटराम अय्यर
- समतुल्य उद्धरण (साइटेशन)– [एआईआर 1958 एससी 538], [1959(61)बीओएमएलआर 192], [1958 आईएनएससी 29], [(1959)आईएमएलजे67], [(1959)1एससी आर279]
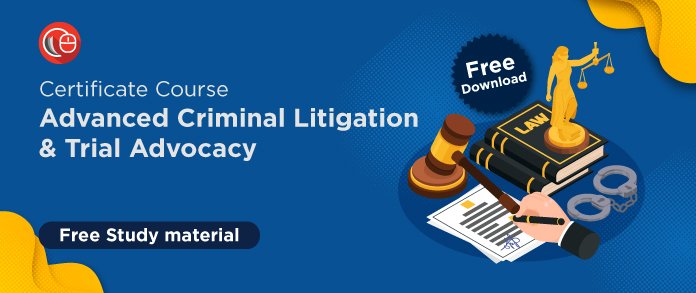
श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर एवं अन्य, 1958 के तथ्य
बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक सामान्य निर्णय के विरुद्ध छह अपीलें की गईं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत तीन विविध आवेदन दायर किए गए, अर्थात्:
- श्री राम कृष्ण डालमिया द्वारा दायर 1957 की संख्या 48;
- श्री श्रेयांस प्रसाद जैन और श्री शीतल प्रसाद जैन द्वारा दायर 1957 की संख्या 49; और
- श्री जय दयाल डालमिया और श्री शांति प्रसाद जैन द्वारा दायर 1957 की संख्या 50।
इन विविध आवेदनों के तहत, वादी ने केंद्र सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना संख्या एसआरओ 2993 दिनांक 11 दिसंबर, 1956 को रद्द करने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना के खंड (10) के अंतिम भाग को छोड़कर अधिसूचना को कानूनी और संवैधानिक रूप से वैध माना।
प्रश्नगत अधिसूचना
अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों के तहत एक जांच आयोग का गठन किया गया, जिसकी अधिसूचना 11 दिसंबर 1956 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण नीचे विस्तार से अध्ययन के लिए दिया गया है:
- रामकृष्ण डालमिया, जयदयाल डालमिया, शांति प्रसाद जैन, श्रीयांस प्रसाद और शीतल प्रसाद जैन जैसे व्यक्तियों तथा उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े उनके रिश्तेदारों या कर्मचारियों द्वारा कई कंपनियों और फर्मों की स्थापना की गई या उनके प्रभाव में काम किया गया। इन कंपनियों ने जनता से पर्याप्त निवेश आकर्षित किया। हालांकि, जांच में वित्तीय हेरफेर सहित उनके प्रबंधन में महत्वपूर्ण अनियमितताएं सामने आईं। यह स्पष्ट हो गया कि जनता द्वारा जुटाए गए धन का एक बड़ा हिस्सा कंपनियों के लाभ के बजाय व्यक्तिगत लाभ की तरफ मोड़ा गया था। नतीजतन, इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप निवेश करने वाली जनता को पर्याप्त वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।
- केंद्र सरकार की राय थी कि इन मामलों की पूरी जांच होनी चाहिए जो सार्वजनिक महत्व के हैं। इसलिए, एक जांच आयोग (जिसे यहां “आयोग” कहा गया है) का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे:
- श्री न्यायमूर्ति एस.आर. तेंदोलकर, बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष;
- मेसर्स ए.एफ. फर्ग्यूसन एंड कंपनी के श्री एन.आर. मोदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सदस्य; और
- श्री एस.सी. चौधरी, आयकर आयुक्त, सदस्य।
3. इस अधिसूचना के तहत 11 बिंदु दिए गए थे, जिन पर आयोग को जांच करनी थी और रिपोर्ट देनी थी। इन 11 में से, खंड (10) सबसे विवादास्पद था जिसने बॉम्बे उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। उच्च न्यायालय के निर्णय से पहले खंड 10 इस प्रकार था:
“(10) जिन कंपनियों और फर्मों के मामलों की जांच आयोग द्वारा की जाती है, उनके संबंध में कोई भी अनियमितता, धोखाधड़ी, या विश्वास का उल्लंघन या ईमानदार वाणिज्यिक प्रथाओं की उपेक्षा या किसी भी कानून का उल्लंघन (उन उल्लंघनों को छोड़कर जिनके संबंध में आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में लंबित है), जो आयोग के ज्ञान में आ सकता है और वह कार्रवाई जो आयोग की राय में निवारण या दंड सुनिश्चित करने या भविष्य के मामलों में निवारक के रूप में की जानी चाहिए।”
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खंड (10) के अंतिम भाग “और कार्रवाई” से लेकर “भविष्य के मामलों में” शब्दों को छोड़कर अधिसूचना को वैध माना और आयोग को निर्देश दिया कि वह जांच को उस सीमा तक आगे न बढ़ाए जहां तक वह खंड (10) के पूर्वोक्त अंतिम भाग से संबंधित है।
4. अधिसूचना के साथ एक अनुसूची संलग्न की गई थी जिसमें 9 कंपनियों और फर्मों के नाम थे जो जांच के दायरे में थीं। इनमें से कुछ कंपनियाँ डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड, डालमिया जैन एविएशन लिमिटेड, सर शापुरजी ब्रोचा मिल्स लिमिटेड, एलन बेरी एंड कंपनी लिमिटेड, इत्यादि थीं।
5. प्रारंभिक अधिसूचना में आयोग द्वारा जाँच पूरी करने के लिए कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था। हालाँकि, 9 जनवरी 1957 को, केंद्र सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 के सभी प्रावधान, जो आयोग को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, लागू होंगे। इसके बाद, 11 फरवरी 1957 को, एक तीसरी अधिसूचना जारी की गई, जिसमें आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा के रूप में तारीख से दो वर्ष निर्दिष्ट किए गए।
श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर और अन्य, 1958 में शामिल कानून
जाँच आयोग अधिनियम, 1952 को 14 अगस्त, 1952 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा इसे लागू किया गया। अधिनियम में जांच आयोग की नियुक्ति तथा ऐसे आयोग को कुछ शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। उपर्युक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:
धारा 3
3(1) यदि कोई उपयुक्त सरकार प्राधिकार रखती है तथा आवश्यक समझे तो वह जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकती है तथा उसे ऐसा लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ही करना होगा। आयोग को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक महत्व के विशिष्ट मामलों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है। हालांकि, यदि एक ही मामले के लिए कई आयोग नियुक्त किए जाते हैं तो कुछ शर्तें हैं, यदि केंद्र सरकार आयोग नियुक्त करती है तो कोई भी राज्य सरकार उसी मामले पर आयोग नियुक्त नहीं कर सकती है तथा यदि राज्य सरकार आयोग नियुक्त करती है तो कोई भी केंद्र सरकार उसी मामले पर आयोग नियुक्त नहीं कर सकती है जब तक कि उसे विश्वास न हो कि जांच कई राज्यों तक विस्तारित होनी चाहिए।
3(2) आयोग में उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त एक या अधिक सदस्य हो सकते हैं तथा जहां आयोग में एक से अधिक सदस्य हों, वहां उनमें से एक को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

3(3) उपयुक्त सरकार किसी भी समय आयोग में उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भर सकती है।
3(4) संबंधित सरकार को जांच के जवाब में की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए आयोग की रिपोर्ट, आयोग द्वारा जांच प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत करनी होगी।
धारा 4
धारा 4 आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमा चलाने के दौरान सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान करती है, जिसमें इसमें निर्दिष्ट कई मामले शामिल हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बुलाना और उसे उपस्थित कराना तथा शपथ पर उसकी जांच करना, किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की मांग करना, शपथपत्र (ऐफिडेविट) पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या अधिकारी से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति मांगना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आयोग जारी करना तथा कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।
धारा 5
धारा 5 आयोग को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करती है:
- यदि उपयुक्त सरकार का मानना है कि जांच की प्रकृति या अन्य परिस्थितियों के कारण आयोग पर कुछ प्रावधान लागू होने चाहिए, तो वह इस आशय की अधिसूचना जारी कर सकती है। निर्दिष्ट प्रावधान तब जारी अधिसूचना के तहत निर्धारित अनुसार आयोग पर लागू होंगे।
- आयोग किसी भी व्यक्ति से जांच से संबंधित जानकारी प्रदान करने की मांग कर सकता है। वह व्यक्ति जानकारी प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
- आयोग या कोई प्राधिकृत अधिकारी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 और धारा 103 के प्रावधानों के अधीन, जांच से संबंधित दस्तावेजों को खोजने, जब्त करने और उद्धरण (एक्सट्रेक्ट) लेने के लिए इमारतों में प्रवेश कर सकता है।
- आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है, यदि कोई व्यक्ति आयोग की उपस्थिति में विशिष्ट अपराध करता है, तो वह अपराध के तथ्यों और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 में दिए गए प्रावधान के अनुसार अभियुक्त के बयान को रिकॉर्ड करने के बाद, मामले को उसी पर सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकता है और जिस मजिस्ट्रेट को ऐसा कोई मामला भेजा जाता है, वह शिकायत की सुनवाई करेगा।
- आयोग के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।
धारा 6
धारा 6 में यह प्रावधान है कि आयोग के समक्ष साक्ष्य देते समय किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी कथन उसे किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाही में उसके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन चलाया जाए, बशर्ते कि कथन किसी ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया गया हो जिसका उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा उससे अपेक्षा की गई हो या जो जांच के विषय-वस्तु से सुसंगत हो।
धारा 7
इस धारा के अंतर्गत समुचित सरकार यह घोषणा करते हुए अधिसूचना जारी कर सकती है कि आयोग अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से अस्तित्व में नहीं रहेगा।
धारा 8
इस धारा के तहत इस अधिनियम या किसी संबंधित नियम या आदेश के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई के लिए सरकार, आयोग, उसके सदस्यों या उनके निर्देशों के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 14
अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है; राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 246
भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 कहता है,
- इस अनुच्छेद के खंड (2) और (3) में किसी भी विरोधाभासी प्रावधानों की परवाह किए बिना संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
- जबकि संसद संघ सूची पर विशेष अधिकार रखती है, यह समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों के लिए राज्य विधानमंडल के साथ विधायी शक्तियों को भी साझा करती है। हालाँकि, टकराव की स्थिति में संसद का अधिकार राज्य के अधिकार से अधिक होता है।
- राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, बशर्ते संसद के विधायी अधिकार या किसी समवर्ती विधायी शक्तियों के साथ कोई टकराव न हो
- संसद के पास भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में सूचीबद्ध मामला हो।

उठाए गए मुद्दे
न्यायालय ने कुछ प्रमुख और मामूली विवादों पर चर्चा की। मुख्य विवाद अधिनियम की संवैधानिकता से संबंधित था।
- क्या अधिसूचना अधिनियम के दायरे से बाहर है या नहीं?
- क्या अधिनियम स्वयं संविधान के दायरे से बाहर है?
- क्या आयोग की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना प्रत्यायोजित अधिकार (डेलिगेटेड अथॉरिटी) की सीमाओं से बाहर है या नहीं?
- क्या अधिनियम और/या अधिसूचना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है या नहीं?
- क्या याचिकाकर्ता की कंपनी को सरकार द्वारा मनमाने ढंग से चुना गया है या नहीं?
पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित अधिसूचना 1952 के जांच आयोग अधिनियम के दायरे से बाहर है।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम स्वयं दो तरह से दायरे से बाहर है। सबसे पहले, यह संसद की क्षमता से बाहर है कि वह इतने व्यापक अधिकार प्रदान करने वाला कानून बनाए और दूसरा, यह जांच न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण है।
- सरकार ने अधिनियम द्वारा दी गई नीतियों और दिशानिर्देशों को ठीक से लागू नहीं किया और अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है।
- सरकार ने याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया है और उन्हें अलग-थलग कर दिया है तथा याचिकाकर्ता को अलग-थलग करने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से अधिसूचना जारी की गई है।
- अधिसूचना और अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।
प्रतिवादी
अधिसूचना अधिनियम की धारा 3 के तहत उल्लिखित शक्तियों से परे नहीं जाती है। अधिनियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि यह अनुच्छेद 246 के दायरे में अधिनियमित किया गया है। संसद या सरकार द्वारा कोई जांच नहीं की गई है, इसलिए न्यायिक कार्यों का कोई अतिक्रमण नहीं है।
श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर एवं अन्य, 1958 में निर्णय
पूरी तरह से अध्ययन के लिए मुद्दावार निर्णय नीचे दिया गया है:
क्या अधिसूचना अधिनियम से परे गई है
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि धारा 3 उचित सरकार को कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच करने के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार देती है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। तर्क यह है कि किसी व्यक्ति या कंपनी का आचरण संभवतः सार्वजनिक महत्व का मामला नहीं हो सकता। इस तर्क को खारिज कर दिया गया और न्यायालय ने कहा कि बड़े बैंकों की विफलता के परिणामस्वरूप आम जनता की जीवन रक्षा का नुकसान निश्चित रूप से सार्वजनिक महत्व का मामला है और ऐसे बैंक के प्रभारी व्यक्तियों और प्रबंधन का आचरण जिसके कारण उसका पतन हुआ, वह भी उतना ही सार्वजनिक महत्व का मामला है। यह पूरी तरह से संभव है कि किसी व्यक्ति या कंपनी या व्यक्तियों या कंपनियों के समूह का आचरण इतना खतरनाक हो सकता है और सार्वजनिक कल्याण पर इतना प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है या पड़ने की धमकी दे सकता है कि ऐसा आचरण सार्वजनिक महत्व का एक निश्चित मामला बन जाए और इसकी पूरी जांच की तत्काल आवश्यकता हो। न्यायालय ने माना कि अधिसूचना धारा 3 द्वारा उपयुक्त सरकार को दी गई शक्तियों के भीतर है।
क्या अधिनियम संविधान के विरुद्ध है
यह तर्क दिया गया कि अधिनियम ने सरकार को भारत के संविधान में उल्लिखित दायरे से परे शक्तियाँ प्रदान की हैं। अधिनियम की वैधता पर दो तरह से सवाल उठाए गए।
सबसे पहले, संसद की विधायी क्षमता से परे, इतने व्यापक अधिकार प्रदान करने वाला कानून बनाना था। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि यदि अधिसूचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, तो अधिनियम स्वयं संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है। संसद ने अनुच्छेद 246 के अनुसार अपने विधायी अधिकार के तहत अधिनियम बनाया, जिसे सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 94 और सूची III में प्रविष्टि 45 के साथ पढ़ा गया। ये प्रविष्टियाँ “जांच” से संबंधित हैं, जो संसद को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देती हैं। हालाँकि, वकील का तर्क है कि संसद की शक्ति को जांच करने तक सीमित रखा जाना चाहिए और अतिरिक्त कार्य प्रदान करने तक विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए। संविधान की व्यापक व्याख्या को स्वीकार करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया कि जांच से संबंधित कानूनों को प्रासंगिक सूचियों के भीतर भविष्य के कानून बनाने में सहायता करने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। वकील का दावा है कि जांच से सार्वजनिक लाभ के लिए या नुकसान को रोकने के लिए नए कानून बनाने के लिए जानकारी एकत्र करने में सुविधा होनी चाहिए। प्रशासनिक जांच या व्यक्तियों को दंडित करने के उद्देश्य से की जाने वाली जांच इन संस्थाओं के दायरे में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि “उद्देश्य के लिए” शब्द यह संकेत देते हैं कि जांच का दायरा आवश्यक रूप से संबंधित सूची में किसी भी प्रविष्टि में विशेष या विशिष्ट मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन मामलों की जांच तक विस्तारित हो सकता है जो उन विशेष मामलों के विधायी या अन्यथा उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

दूसरा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जांच न तो किसी विधायी या प्रशासनिक उद्देश्य के लिए थी, बल्कि यह न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण था। यह तर्क दिया गया कि संसद कथित व्यक्तिगत गलतियों या निजी विवादों की जांच नहीं कर सकती क्योंकि ऐसी जांच स्पष्ट रूप से कानून के सहायक नहीं है। यह तर्क दिया गया कि यदि आपराधिक मुकदमा चलाया जाना है, तो प्रारंभिक जांच आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अनुसार होनी चाहिए और किसी भी विधायिका को अपने आप जांच शुरू करने और इस तरह नागरिक को सीआरपीसी के प्रावधानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य सुरक्षा से वंचित करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और अधिसूचना के खंड (10) का वह हिस्सा हटा दिया गया जो अधिकार-विहीन (अल्ट्रा वायरस) था। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की, लेकिन जिस तर्क पर निष्कर्ष आधारित था, उसे अस्वीकार कर दिया गया। न्यायालय ने कहा कि न तो संसद और न ही सरकार ने कोई जांच की है। संसद ने जांच से संबंधित कानून बनाया है और अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट कुछ परिस्थितियों में जांच आयोग गठित करने का काम उपयुक्त सरकार पर छोड़ दिया है। बदले में, केंद्र सरकार ने अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस आयोग का गठन किया है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि संसद या सरकार ने स्वयं कोई जांच करने का बीड़ा उठाया है। इसके बाद, यह तर्क कि आयोग को दी गई शक्तियां न्यायपालिका में निहित शक्तियों में बाधा डालती हैं, को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। संबंधित आयोग का गठन केवल जांच करने और अपने निष्कर्षों और सिफारिशों को दर्ज करने के लिए किया गया है, उन्हे जांच या रिपोर्ट को न्यायिक कार्य के अभ्यास के अर्थ में न्यायिक जांच के रूप में नहीं देखा जा सकता है और परिणामस्वरूप, इस मामले के तथ्यों के आधार पर संसद या सरकार द्वारा भारत संघ के न्यायिक अंगों की शक्तियों का हड़पने का प्रश्न ही नहीं उठता।
क्या अधिनियम और/या अधिसूचना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है
अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के वास्तविक अर्थ को समझाने के लिए बुधन चौधरी बनाम बिहार राज्य (1954) मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14 नस्ल या धर्म जैसे कुछ कारकों के आधार पर अनुचित व्यवहार की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह कानून बनाने के उद्देश्य से उचित भेदभाव की अनुमति देता है। उचित माने जाने के लिए, इन भेदभावों को दो शर्तों को पूरा करना होगा:
- यह वर्गीकरण एक सुस्पष्ट अंतर पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहीकृत किए गए व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से अलग करता है, और
- यह अंतर उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रखता है जिसे संबंधित कानून द्वारा प्राप्त किया जाना है।
बुधन चौधरी मामले में न्यायालय ने कहा कि जो आवश्यक है वह यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए।
न्यायालय ने 5 श्रेणियों के बारे में बताया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत वैधता पर सवाल उठाने वाला कानून आएगा। इन 5 श्रेणियों को नीचे विस्तार से समझने के लिए संक्षेप में बताया गया है:
- एक कानून यह निर्दिष्ट कर सकता है कि यह किस पर लागू होता है और क्यों कुछ लोगों या चीजों को इसमें शामिल किया जाता है जबकि अन्य को नहीं। इस वर्गीकरण को या तो सीधे कानून में बताया जा सकता है या इसके आसपास के संदर्भ से अनुमान लगाया जा सकता है। यह तय करते समय कि क्या ऐसा कानून वैध है, न्यायालय यह देखता है कि क्या यह वर्गीकरण उचित है और कानून के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून विशिष्ट व्यक्तियों या समूह को लक्षित करता है; महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वर्गीकरण इन मानदंडों को पूरा करता है। यदि ऐसा है, तो न्यायालय कानून को वैध मानेगा। न्यायालय ने फिर चिरंजीत चौधरी बनाम भारत संघ (1950) के मामले का हवाला दिया, जिसमें उसने शोलापुर और वीविंग कंपनी (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम को बरकरार रखा, यह फैसला सुनाया कि यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है और केवल शेयरधारकों की शक्तियों का प्रबंधन करता है।
- कभी-कभी, कोई कानून कानून में या आसपास की परिस्थितियों से स्पष्ट वर्गीकरण के लिए किसी स्पष्ट या उचित आधार के बिना एक व्यक्ति या चीज या कई व्यक्तियों या चीजों को लक्षित कर सकता है। ऐसे मामलों में, यदि न्यायालय को वर्गीकरण के लिए उचित औचित्य नहीं मिल पाता है, तो वह कानून को भेदभावपूर्ण घोषित कर देगा। न्यायालय ने अमीरुन्निसा बेगम एवं अन्य बनाम महबूब बेगम एवं अन्य (1952) के मामले का हवाला दिया, जो वलीउद्दौला उत्तराधिकार अधिनियम, 1950 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी भेदभावपूर्ण प्रकृति और अधिकार के दुरुपयोग के कारण असंवैधानिक पाया था।
- कभी-कभी, कोई कानून निर्दिष्ट नहीं करता है कि यह किस पर लागू होता है, जिससे यह तय करना सरकार पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय सिर्फ इसलिए कानून को स्वतः रद्द नहीं कर देगा क्योंकि इसमें वर्गीकरण शामिल है या सरकार को विवेकाधिकार दिया गया है। इसके बजाय, न्यायालय यह जांच करेगा कि क्या कानून में सरकार के लिए निर्णय लेते समय पालन किये जाने हेतु कोई सिद्धांत या दिशानिर्देश स्थापित किये गये हैं। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है और यह सरकार को भेदभाव करने का मनमाना अधिकार देता है, तो वह कानून को अवैध घोषित कर देता है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 को अमान्य घोषित कर दिया था और न्यायालय ने माना था कि इस अधिनियम के तहत प्रावधान राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना मामलों को वर्गीकृत करने का अनियंत्रित अधिकार प्रदान करते हैं।
- कभी-कभी, कोई क़ानून अपने प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से व्यक्तियों या चीज़ों का वर्गीकरण नहीं कर सकता है और व्यक्तियों या चीज़ों को वर्गीकृत करने का काम सरकार पर छोड़ सकता है। हालाँकि, यह उसी समय वर्गीकरण के लिए सरकार के लिए कोई नीति या सिद्धांत निर्धारित कर सकता है, और न्यायालय कानून को संवैधानिक रूप से बनाए रखेगा।
- कभी-कभी, कोई कानून यह निर्दिष्ट नहीं कर सकता है कि यह किस पर लागू होता है, इसलिए कानून में उल्लिखित सिद्धांतों या नीतियों के आधार पर निर्णय लेना सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। यदि सरकार अपने निर्णय लेते समय इन नीतियों का पालन नहीं करती है, तो न्यायालय सरकार के कार्यों को अमान्य मानेगा, न कि कानून को, जैसा कि उसने काठी रानिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य (1952) के मामले में किया था।

अब, सवाल यह उठता है कि विवादित अधिनियम या अधिसूचना किस श्रेणी में आती है?
अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि इसके शीर्षक से स्पष्ट है, जांच आयोगों की स्थापना करना और उन्हें विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करना है। अधिनियम की धारा 3 उपयुक्त सरकार को सार्वजनिक महत्व के किसी विशिष्ट मामले की जाँच करने के लिए कुछ परिस्थितियों में जाँच आयोग नियुक्त करने का अधिकार देती है। इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि यह जाँच मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक होनी चाहिए और स्वतंत्र नहीं हो सकती। इस शक्ति का दायरा सार्वजनिक महत्व के मामलों की जाँच तक सीमित है, जो एक स्पष्ट वर्गीकरण को दर्शाता है। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम उपर्युक्त चौथी श्रेणी के दायरे में आता है, यदि पहली नहीं, और सरकार को मनमानी शक्ति नहीं सौंपता है, जिससे यह मौजूदा कानूनी मिसालों के आधार पर संवैधानिक रूप से वैध हो जाता है।
क्या आयोग की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना प्रत्यायोजित अधिकार की सीमाओं से परे है
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि भले ही अधिनियम को वैध माना जा सकता है, लेकिन सरकार ने उचित वर्गीकरण के आधार पर अपने विवेक का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है, जिसका अर्थ है कि अधिनियम ने स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, और सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग करते समय उनका उचित रूप से पालन नहीं किया है। यह तर्क भारतीय कंपनी अधिनियम का आकलन करने के लिए श्री त्रिकमदास द्वारकादास और श्री थिरुवेंकटचारी की नियुक्ति के बाद की घटनाओं के अनुक्रम से उपजा है। बाद की जांच और पुनर्प्रकाशन के बावजूद, जिसमें भाभा समिति द्वारा की गई जांच भी शामिल है, जिसने कंपनी अधिनियम के पुनर्गठन में योगदान दिया, याचिकाकर्ता आगे की जांच की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। उनका तर्क है कि चूंकि समिति की रिपोर्ट के बाद कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं हुआ है, इसलिए अतिरिक्त जांच की कोई स्पष्ट आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने दो आधारों पर इस तर्क से असहमति जताई, पहला, भाभा समिति ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 29 पर सिफारिश की है कि भविष्य में कंपनियों से संबंधित कुछ मामलों के बारे में और जांच की जानी चाहिए, और इसलिए नई जांच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, उपयुक्त सरकार को जांच आयोग नियुक्त करने का अधिकार है, यदि उसकी राय में वह इसे आवश्यक समझे।
क्या याचिकाकर्ता की कंपनियों को मनमाने ढंग से जांच के लिए चुना गया है?
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उन्हें और उनकी कंपनियों को भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए गलत तरीके से निशाना बनाया गया है और उन्हें बोझिल जांच के अधीन किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने का निर्णय लेने के बाद से ही भेदभाव शुरू हो गया था। वे भाभा समिति के समक्ष बॉम्बे शेयरहोल्डर एसोसिएशन द्वारा दायर ज्ञापन की ओर इशारा करते हैं, जिसमें अन्य व्यवसायियों और कंपनियों के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। आरोपों में इन समानताओं के बावजूद, सरकार ने याचिकाकर्ताओं और उनकी कंपनियों पर चुनिंदा तरीके से अधिनियम लागू किया और उनके खिलाफ अधिसूचना जारी की, जबकि अन्य को बाहर रखा। जबकि अधिसूचना मुख्य रूप से याचिकाकर्ता और उनकी कंपनियों को प्रभावित करती है, याचिकाकर्ता का तर्क है कि संसद ने अधिनियम के चुनिंदा आवेदन को उपयुक्त सरकार के विवेक पर छोड़ दिया है। इसलिए, सरकार के निर्णय उपलब्ध साक्ष्य और गठित राय पर आधारित होने चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनका व्यवहार मनमाना और अनुचित था। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि उपयुक्त सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री की सच्चाई की न्यायिक जांच करे। इसके बजाय, उसे उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करना चाहिए और अपने विवेक का ईमानदारी से प्रयोग करना चाहिए। जबकि व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की चिंताएँ हो सकती हैं, लेकिन यदि कानून का गलत तरीके से या अयोग्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो उन्हें न्यायालय में संबोधित किया जा सकता है। इस मामले में, केंद्र सरकार ने जांचकर्ताओं को नियुक्त किया और विभिन्न रिपोर्टों और ज्ञापनों तक पहुँच प्राप्त की, इससे पहले कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि याचिकाकर्ता के आचरण की जाँच उसके कथित सार्वजनिक महत्व के कारण आवश्यक थी। न्यायालय ने संकेत दिया कि आरोप के कानूनी साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है, मुख्य प्रश्न यह है कि यदि आरोपों पर सद्भावनापूर्वक विश्वास किया जाए, तो क्या वे सार्वजनिक महत्व के मामले हैं और न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में, वास्तव में वे हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यह याचिकाकर्ताओं पर निर्भर है कि वे संदेह से परे आरोप लगाएँ और साबित करें कि अन्य व्यक्तियों या कंपनियों को छोड़ दिया गया है और याचिकाकर्ताओं और उनकी कंपनियों को भेदभावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए चुना गया है। हालाँकि, न्यायालय की राय में याचिकाकर्ता अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहे।
अंततः, न्यायालय ने अधिसूचना और अधिनियम दोनों को वैध माना। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि खंड (10) के उत्तरार्द्ध (लैटर) भाग में आने वाले शब्द “निवारण या दंड के माध्यम से” हटा दिए जाएंगे और उन्हें इस प्रकार पढ़ा जाएगा: “और आयोग की राय में जो कार्रवाई की जानी चाहिए… भविष्य के मामलों में निवारक के रूप में कार्य करने के लिए”।
निर्णय के पीछे तर्क
इस मामले में, निर्णय के पीछे न्यायालय के तर्क को कई प्रमुख पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें पृथक्करण (सेपरेशन) का सिद्धांत और अनुच्छेद 14 के कथित उल्लंघन का विश्लेषण शामिल है।
सबसे पहले, न्यायालय ने निर्णय के परिच्छेद (पैराग्राफ) 12 में पृथक्करण के सिद्धांत को संबोधित किया, विशेष रूप से अधिसूचना के खंड (10) से कुछ शब्दों को हटाने के संबंध में। न्यायालय ने उच्च न्यायालय के तर्क से सहमति व्यक्त की कि शब्दों को हटाने के बावजूद अधिसूचना की प्रभावशीलता बरकरार रही। इसने निष्कर्ष निकाला कि हटाए गए शब्दों ने अधिसूचना की कार्यक्षमता को प्रभावित नहीं किया। इसके अलावा, न्यायालय ने प्रासंगिक मामलों, कानूनों और कानूनी सिद्धांतों की गहन जांच के माध्यम से अनुच्छेद 14 के कथित उल्लंघन पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जांच आयोग की नियुक्ति के प्रावधान सहित अधिनियम अनुच्छेद 13 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आयोग स्थापित करने का सरकार का निर्णय उचित था और स्थापित दिशानिर्देशों और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार संचालित किया गया था। यह कानूनी व्याख्याओं के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, विधायी इरादे के संरक्षण को सुनिश्चित करता है और समानता और उचित प्रक्रिया के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखता है।

संदर्भित उदाहरण
बुधन चौधरी बनाम बिहार राज्य (1954) पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय के विरुद्ध अपील थी, जिसमें संविधान के संबंध में विधि का प्रश्न उठाया गया था। यह अपील बिहार में आयोजित एक आपराधिक मुकदमे से उत्पन्न हुई थी। अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई थी और फिर उन पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 30 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ताओं पर सत्र न्यायालय की बजाय धारा 30 के मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, तथा उन्हें भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपों में दोषी ठहराया गया था। अपीलकर्ताओं ने संविधान के उल्लंघन के आधार पर पटना उच्च न्यायालय में अपील की थी। अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि धारा 30 संविधान के अनुच्छेद 14 (भेदभाव न करना) का उल्लंघन नहीं करती है। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा कम कर दी। न्यायालय ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी। इस मामले में, न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के परिच्छेद 13 के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए निर्णय का संदर्भ दिया।
इसके बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के कथित उल्लंघन की जांच की और यह आकलन करने के लिए 5 श्रेणियों को रेखांकित किया कि क्या कोई कानून इस संवैधानिक प्रावधान का संभावित रूप से उल्लंघन कर सकता है। न्यायालय ने प्रत्येक श्रेणी के लिए कई मामले का हवाला दिया, जिन्हें नीचे संक्षेप में बताया गया है:
- पहली श्रेणी के तहत, एक क़ानून स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों या चीज़ों को निर्दिष्ट कर सकता है जिन पर इसके प्रावधान लागू होते हैं और इसके पीछे का तर्क और इसे वैध माना जाएगा। इसके लिए, न्यायालय ने चिरंजीत चौधरी बनाम भारत संघ (1950) के निर्णय का संदर्भ दिया। चिरंजीत लाल चौधरी के मामले में, शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड के एक शेयरधारक ने एक याचिका दायर की। भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा शासित कंपनी को कुप्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता जैसे कारणों से अगस्त 1949 में बंद होने का सामना करना पड़ा। इसके बाद, सरकार ने शोलापुर एंड वीविंग कंपनी (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम पारित किया, जिससे कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए उसे व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। इसमें नए निर्देशक नियुक्त करना, शेयरधारकों के मताधिकार में कटौती करना और कंपनी पर लागू भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करना शामिल था। चौधरी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(f) और 31 का आरोप लगाते हुए अध्यादेशों और अधिनियम दोनों की संवैधानिकता को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला सुनाया और निष्कर्ष निकाला कि यह याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। दिए गए तर्क के अनुसार अधिनियम में कंपनी की संपत्ति का अधिग्रहण शामिल नहीं था और न ही यह याचिकाकर्ता को उसके मूल अधिकारों के आनंद से वंचित करता था। जबकि अधिनियम ने मतदान के अधिकारों में कटौती की, इसने शेयर रखने और आय प्राप्त करने की उनकी क्षमता को बाधित नहीं किया और अपील को खारिज कर दिया गया।
- दूसरी श्रेणी के तहत, एक क़ानून वर्गीकरण के लिए स्पष्ट तर्क के बिना विशिष्ट व्यक्तियों या जांघों को लक्षित कर सकता है। यदि कानून में विभेदीकरण के लिए उचित आधार का अभाव है और वह अनुचित रूप से भेदभाव करता प्रतीत होता है, तो न्यायालय इसे असंवैधानिक पा सकता है। न्यायालय ने अमीरुन्निसा बेगम एवं अन्य बनाम महबूब बेगम एवं अन्य (1952) के मामले का हवाला दिया, जो वलीउद्दौला उत्तराधिकार अधिनियम, 1950 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। यह कानून नवाब वलीउद्दौला की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य दिवंगत नवाब की दो पत्नियों महबूब बेगम और कादरियन और उनके बच्चों द्वारा रखे गए उत्तराधिकार के दावों को खारिज करना था। विवाद शादियों की वैधता और नवाब की संपत्ति पर हक को लेकर उठा। इस अधिनियम को भेदभावपूर्ण होने और राजप्रमुख सत्ता को कोसने के लिए चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण किया और पाया कि यह अधिनियम भेदभावपूर्ण प्रकृति और सत्ता के दुरुपयोग के कारण असंवैधानिक है।
- तीसरी श्रेणी के तहत, कोई क़ानून सरकार को अपने आवेदनों के लिए व्यक्तियों का चयन करने का विवेक प्रदान कर सकता है। न्यायालय यह जाँच करेगा कि क्या क़ानून इस विवेक का मार्गदर्शन करने वाला कोई सिद्धांत या नीति प्रदान करता है; यदि नहीं, तो सरकार द्वारा मनमाने ढंग से भेदभाव करने के लिए इसे रद्द किया जा सकता है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) के मामले का उल्लेख किया, इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल विशेष न्यायालय अधिनियम, 1950 को अमान्य कर दिया। न्यायालय ने माना कि इस अधिनियम के तहत प्रावधान राज्य सरकार को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बिना मामलों को वर्गीकृत करने का अनियंत्रित अधिकार प्रदान करते हैं। शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता को स्वीकार करने के बावजूद, न्यायालयों ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की भाषा मनमाने वर्गीकरण की अनुमति देती है, तथा वर्गीकरण और अधिनियम के उद्देश्य के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। अपराधों को वर्गीकृत करने में अधिनियम की कमी और सीआरपीसी के वर्गीकरण सिद्धांत को शामिल करने में इसकी विफलता ने इसे संवैधानिक रूप से अमान्य बना दिया।
- चौथी और पाँचवीं श्रेणियों के लिए, न्यायालय ने काठी रानिंग रावत बनाम सौराष्ट्र राज्य (1952) के मामले का उल्लेख किया। इस मामले में अपीलकर्ता ने सौराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुरक्षा उपाय अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी, जो विशिष्ट गंभीर अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयो की स्थापना की अनुमति देता है। अपीलकर्ता के इस तर्क के बावजूद कि विधि अध्यादेश मनमाना वर्गीकरण करके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यादेश की वैधता बरकरार रखी। न्यायालय ने तर्क दिया कि विशेष न्यायालयों द्वारा परीक्षण के लिए अपराधों और व्यक्तियों का वर्गीकरण उचित अंतर पर आधारित था और सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के वैध उद्देश्य को पूरा करता था। अनवर अली सरकार मामले के साथ एक समानांतर रेखा खींचते हुए, जहां एक समान कानून को संबंध की कमी के कारण रद्द कर दिया गया था, न्यायालय ने पाया कि काठी के मामले में चुनौती दिए गए कानून के पास इसके वर्गीकरण के लिए स्पष्ट आधार और औचित्य था।
श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर एवं अन्य, 1958 का आलोचनात्मक विश्लेषण
इस मामले में निर्णय, 1952 के जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच आयोग की भूमिका और कार्य के बारे में कई प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आयोग तथ्य एकत्र कर सकता है और जांच कर सकता है, लेकिन वह सरकार को विधायी या कार्यकारी उपाय नहीं सुझा सकता है। हालांकि, न्यायालय ने असहमति जताते हुए पहचाने गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए विधायी या प्रशासनिक कार्रवाइयों के संबंध में सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करने में आयोग की सिफारिश के महत्व पर जोर दिया। आयोग के पास न्यायिक शक्तियों की कमी और इसकी रिपोर्टों की विशुद्ध रूप से सिफारिशी प्रकृति के बावजूद, न्यायालय ने सरकारी कार्यों का मार्गदर्शन करने में इसकी सिफारिशों के महत्व को स्वीकार किया। इसके साथ ही, निर्णय ने संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की फिर से पुष्टि की। इसने रेखांकित किया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के अलग-अलग अंग हैं, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। न्यायालय ने इस सिद्धांत को प्रतिबंधात्मक रूप से लागू किया, प्रत्येक अंग की अलग-अलग भूमिकाओं पर जोर दिया और दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को खारिज कर दिया।
जिस निर्णय के लिए इस मामले पर भरोसा किया गया
अमर जोती बिल्डर्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1972)
इस रिट याचिका में, 28 ईंट भट्ठा मालिकों ने दिल्ली ईंट नियंत्रण आदेश, 1963 और संबंधित निर्देशों के विभिन्न पहलुओं पर विवाद किया, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। हालाँकि शुरू में कई प्रावधानों को चुनौती दी गई, लेकिन कार्यवाही के दौरान ध्यान बदल गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गैर-उपभोक्ताओं को ईंटें बेचने पर प्रतिबंध तो था, लेकिन उसने पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया। इसके अलावा, उसने समय-समय पर समीक्षा और लागत वृद्धि जैसे कारकों पर विचार करते हुए मूल्य निर्धारण को उचित पाया। खंड 6 के संबंध में, न्यायालय ने तर्क दिया कि यह कानून के ढांचे के भीतर काम करता है और निरंकुश शक्ति प्रदान नहीं करता है। नतीजतन, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, और प्रत्येक पक्ष को अपनी-अपनी लागतों को सम्मिलित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि धारा 6(1) शुरू में अनियंत्रित अधिकार प्रदान करती प्रतीत होती है, लेकिन आदेश और अधिनियम के व्यापक संदर्भ में इसकी व्याख्या से पता चलता है कि इसके द्वारा अधिकृत निर्देश ईंटों के वितरण, बिक्री और परिवहन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के अनुरूप होने चाहिए। इस व्याख्या का समर्थन राम कृष्ण डालमिया मामले में किया गया। न्यायालय ने पाया कि धारा 6 कानून के दायरे में काम करती है।

निष्कर्ष
अंत में, श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदोलकर एवं अन्य ने अधिनियम की संवैधानिकता और इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता के बारे में जटिल कानूनी प्रश्न प्रस्तुत किए। पृथक्करण के सिद्धांत और अनुच्छेद 14 के कथित उल्लंघन सहित विभिन्न कानूनी सिद्धांतों की सावधानीपूर्वक जांच के माध्यम से, न्यायालय ने अधिसूचनाओं और अधिनियम दोनों की वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय के निर्णय ने विधायी मंशा और संवैधानिक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के कथित उल्लंघन को अमान्य करने के लिए कई मामलों का हवाला दिया, जिसे अंत में स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
“न्यायिक शक्तियों का हड़पना” वाक्यांश का क्या अर्थ है?
भारत का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का पालन करता है, जो सरकार की प्रत्येक शाखा के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निहित इस सिद्धांत का उद्देश्य प्रत्येक सरकार को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करके अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। यह अनिवार्य करता है कि कोई भी शाखा अपने निर्दिष्ट अधिकार से आगे नहीं बढ़ सकती। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जांच आयोग को निजी विवादों और व्यक्तियों की जांच करने और उनके निष्कर्षों के आधार पर दंड की सिफारिश करने का अधिकार देना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है और न्यायिक शक्तियों की सीमाओं का अतिक्रमण है।
पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है?
पृथक्करणीयता के सिद्धांत का अर्थ है कि जब किसी क़ानून का कोई विशेष प्रावधान संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध है, लेकिन वह प्रावधान क़ानून के बाकी हिस्सों से अलग करने योग्य है, तो केवल उस उल्लंघनकारी प्रावधान को ही न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा, न कि पूरे क़ानून को। यदि अच्छे और बुरे प्रावधानों को ‘और’ या ‘या’ शब्दों का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता है और अच्छे प्रावधान के प्रवर्तन को बुरे प्रावधान के प्रवर्तन पर निर्भर नहीं बनाया जाता है, अर्थात अच्छे प्रावधान को लागू किया जा सकता है, भले ही बुरा प्रावधान मौजूद न हो या मौजूद न हो, दोनों प्रावधान अलग-अलग हैं और अच्छे प्रावधान को वैध माना जाएगा और उसे प्रभावी बनाया जाएगा।
संदर्भ







