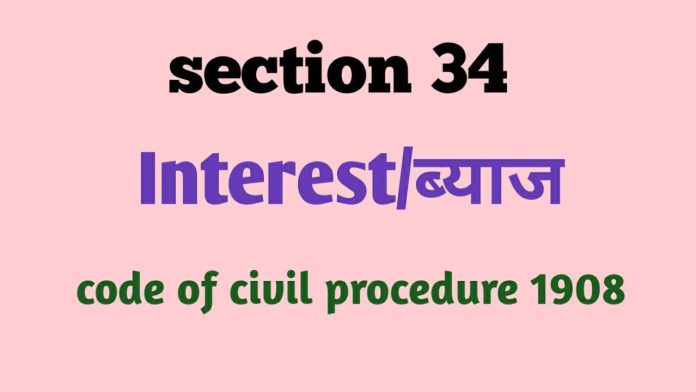यह लेख दिल्ली के इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के विवेकानंद व्यावसायिक अध्ययन संस्थान के छात्र Sarthak Mittal द्वारा लिखा गया है। यह बताता है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 के तहत अदालतें दीवानी मामलों में कैसे ब्याज लगा सकती हैं। इस लेख का अनुवाद Shubhya Paliwal द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
ब्याज डिक्री-धारक (डिक्री होल्डर) को देय धन (ड्यू मनी) से वंचित होने के लिए दिए गए मुआवजे (कंपनसेशन) की तरह है। ब्याज का दावा उस क्षण (मोमेंट) से किया जा सकता है जिस क्षण से डिक्री-धारक को भुगतान किया जाना था और जब तक कि उसे भुगतान नहीं कर दिया गया। हालांकि, ब्याज का दावा करने के अधिकार से संबंधित विभिन्न अर्थों को समझना उचित है, जिसमें यह भी शामिल है कि ब्याज की दर कैसे तय की जाएगी, क्या यह डिक्री-धारक का गैर-अपमानजनक अधिकार है, और क्या किसी अवधि के लिए ब्याज को वर्जित किया जाएगा या नहीं। दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34, वह प्रावधान है जो आम तौर पर धन के भुगतान के लिए पारित की गई डिक्री के संबंध में अदालत द्वारा ब्याज के अधिनिर्णय (अवार्ड) से संबंधित सभी नियमों का प्रतीक है।
ब्याज क्या है
भारतीय स्टेट बैंक बनाम विजय लक्ष्मी ठकराल (2011), के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने “ब्याज” शब्द की परिभाषा की व्याख्या की जिसमें उसने रिचेस बनाम वेस्टमिंस्टर बैंक लिमिटेड (1947), मामले में लॉर्ड राइट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने “ब्याज” को उस भुगतान के रूप में परिभाषित किया जो लेनदार (क्रेडिटर) द्वारा देय तिथि पर पैसा नहीं होने पर दिया जाता है। इसे उस लाभ के रूप में माना जा सकता है जो देनदार (डेटर) को नियत तारीख पर पैसा मिल सकता था; इसके विपरीत, वह लेनदारों के कारण नुकसान उठाता है और ब्याज लगाकर मुआवजा दिया जाता है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए, तो यहां की अदालत “टाइम वैल्यू ऑफ मनी” की अवधारणा को मान्यता देती है, जो यह बताती है कि आज हमारे हाथ में जो पैसा है, वह भविष्य में उसी राशि से कम है। यह मुद्रास्फीति (इनफ्लेशन) के कारण होता है जो कुछ समय के लिए धन की क्रय क्षमता (बाइंग कैपेसिटी) को कम कर देता है और धन की शक्ति के कारण लाभ कमाने के लिए निवेश किया जाता है। सभी मामलों में, यदि किसी को अनुचित रूप से पैसे से वंचित रखा जाता है, तो वह ब्याज सहित मुआवजे का हकदार है, क्योंकि प्रत्येक बीतते दिन के साथ पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाती है और वह ऐसे पैसे से निवेश करने और लाभ कमाने का अवसर खो देता है।
ब्लैक लॉ डिक्शनरी (चौथा संस्करण (एडिशन) में, पैसे के संबंध में “ब्याज” शब्द को पीबॉडी बनाम बीच (1856) के मामले के अनुरूप (कंसोनेंस) परिभाषित किया गया है। कानून द्वारा अनुमत मुआवजे के रूप में या पैसे के उपयोग या मनाही या रोक के लिए पक्षकारों द्वारा तय किया गया, जबकि, पक्षकारों के समझौते द्वारा तय किए गए ब्याज को पारंपरिक ब्याज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कानून द्वारा प्रदान किए गए ब्याज के अभाव में कानूनी ब्याज के रूप में ब्याज को निर्धारित करने वाला स्पष्ट शब्द, जिसे आगे “साधारण ब्याज” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें मूल राशि का एक विशिष्ट प्रतिशत ब्याज के रूप में प्रदान किया जाता है, और “चक्रवृद्धि (कंपाउंड) ब्याज”, जिसमें ब्याज की गणना एक विशिष्ट अवधि के लिए की जाती है और फिर मूल योग में जोड़ा जाता है, और बाद में वह योग नया मूलधन बन जाता है।
उपयोगी ऋण अधिनियम, 1918 की धारा 2(1) के तहत में शब्द “ब्याज” को परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत वास्तव में जो उधार दिया गया था, उससे अधिक रिटर्न शामिल है, इस अतिरिक्त को विशेष रूप से ब्याज के रूप में या अन्यथा किसी अन्य तरीके से चार्ज किया जा सकता है या पुनर्प्राप्त करने की मांग की जा सकती है।
सीपीसी की धारा 34: एक सिंहावलोकन (ओवरव्यू)
जब एक अदालत एक डिक्री पारित करती है, तो अदालत उस राशि पर ब्याज दे सकती है जिसके लिए डिक्री-धारक को हकदार पाया जाता है, और धारा 34 इस तरह के ब्याज को देने से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान प्रदान करती है। धारा उस राशि को स्पष्ट करती है जिस पर ब्याज दिया जाता है, जिसे “मूल राशि अधिनिर्णित” कहा जाता है। इसमें मूल राशि शामिल है, जिसके लिए डिक्री धारक हकदार है, साथ ही वाद को संस्थित (इंस्टीट्यूट) करने से पहले की अवधि के लिए ऐसी राशि पर लगाए गए ब्याज के साथ नतीजतन, सामान्य तौर पर, यह वाद दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा अदालत में दावा की गई पूरी राशि है, जिसके लिए वह वाद दायर करने से पहले हकदार हो जाता है।
इसके अलावा, धारा 34 की उपधारा (1) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है क्योंकि इसमें दो प्रकार की अवधियों पर ब्याज दिए जाने का प्रावधान है जो इस प्रकार हैं: –
- वाद की तिथि से डिक्री की तिथि तक: अधिनिर्णित मूल राशि पर ब्याज वाद की तिथि से डिक्री की तिथि तक है। ब्याज दर अदालत के विवेक पर होनी चाहिए और इस तरह के ब्याज की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- डिक्री की तारीख से डिक्री धारक को पैसे के भुगतान की तारीख तक: यहां, अदालत अपने विवेक से अधिनिर्णित मूल राशि पर ब्याज दे सकती है। हालाँकि, इस तरह की ब्याज दर पर एक ऊपरी सीमा धारा द्वारा तय की गई है जो छह प्रतिशत प्रति वर्ष है; इस तरह के ब्याज को “अतिरिक्त ब्याज” कहा जाता है। इस उपधारा के प्रावधान में दिया गया है कि वाणिज्यिक (कमर्शियल) लेनदेन के मामले में आगे ब्याज छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अधिक हो सकता है और ऐसे मामलों में ऊपरी सीमा ब्याज की संविदात्मक दर होगी। परन्तुक आगे स्पष्ट करता है, कि जहां ब्याज की कोई संविदात्मक दर नहीं है बशर्ते ऊपरी सीमा वह दर होगी जिस पर वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में राष्ट्रीयकृत (नेशनलाइज्ड) बैंकों द्वारा पैसा उधार दिया जाता है या दिया जाता है।
परंतुक की पहली व्याख्या प्रदान करती है कि “राष्ट्रीयकृत बैंकों” शब्द का अर्थ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार माना जाता है, जिसमें अधिनियम ने एक बैंक को “संबंधित नए बैंक” के रूप में वर्गीकृत किया है।” “संबंधित नए बैंक” शब्द को अधिनियम की धारा 2 (d) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बैंकों के रूप में सूचीबद्ध निकाय कॉर्पोरेट्स की सूची है, और ऐसे निकाय कॉरपोरेट्स की सूची अधिनियम की पहली अनुसूची के कॉलम संख्या 2 के तहत प्रदान की गई है।
परंतुक की दूसरी व्याख्या यह प्रदान करती है कि “वाणिज्यिक लेन-देन” शब्द उन लेन-देन को संदर्भित करेगा जो उस पक्ष के उद्योग (इंडस्ट्री), व्यापार या व्यवसाय से जुड़े हैं, जिसने दायित्व वहन किया है। यह ध्यान रखना उचित है कि जिस पक्ष ने दायित्व वहन किया है वह निर्णायक ऋणी (जजमेंट डेटर) होगा। धारा 34 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि जहां न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी है लेकिन आगे ब्याज देने पर डिक्री मौन है, तो यह समझा जाना चाहिए कि न्यायालय ने ऐसे ब्याज से इनकार कर दिया है। निम्नलिखित प्रावधान इस तरह के ब्याज का दावा करने के लिए बाद के मुकदमे को भी रोकता है।
सीपीसी की धारा 34 का दायरा
भगवंत जेनुजी बनाम गंगाबिसन रामगोपाल (1940) के मामले के अनुसार, यह माना गया था कि धारा 34 केवल उन मामलों में लागू होती है जहां डिक्री पैसे के भुगतान के लिए है, और तथ्य यह है कि वाद में अनिर्णीत नुकसान या परिनिर्धारित (अनलिक्विडेटिड) नुकसान के दावे शामिल हैं, वे इस धारा के आवेदन के लिए महत्वहीन है। इसके अलावा, द्वारकानाथ बनाम देबेंद्र (1906), के मामले में यह माना गया था कि मध्यवर्ती लाभ (मेसने प्रॉफिट) और धारा 34 के बीच कोई समानता नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि पूर्व का उद्देश्य गलत तरीके से कब्जे से होने वाले नुकसान की स्थिति का उपचार करना है और बाद का उद्देश्य फैसले के कर्जदार के अन्यायपूर्ण संवर्धन को लंबे समय तक सुधारना है।
यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 34 उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां डिक्री एक बंधक या शुल्क के प्रवर्तन के लिए है क्योंकि यह संहिता के आदेश 34 नियम 11 द्वारा शासित है। हालांकि, आदेश 34 नियम 6 के तहत पारित एक डिक्री, जो देय राशि से संबंधित है, जब बंधक संपत्ति की बिक्री से आय एक बंधक के बदले में दिए गए ऋण को कवर करने के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, तो धारा 34 द्वारा शासित होती है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत डिक्री है।
धारा 34 सीपीसी में संशोधन
संशोधन अधिनियम, 1956
1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 34 में संशोधन किया गया, जिसमें “अतिरिक्त ब्याज” की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों को प्रतिस्थापित (सबस्टिट्यूट) किया गया और ऐसे ब्याज पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की रोक जोड़ी गई। निम्नलिखित संशोधन ने उप-धारा (2) में “कुल योग” शब्दों को “मूल राशि” शब्दों से प्रतिस्थापित किया।
संशोधन अधिनियम, 1976
धारा 34 को बाद में 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें प्रावधान में और दो स्पष्टीकरण प्रदान किए गए थे जो उन मामलों में स्पष्टता प्रदान करते थे जहां वाणिज्यिक लेनदेन में और ब्याज दिया जाना था। संशोधन अधिनियम की धारा 97 (e) में प्रावधान है कि वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में धारा 34 में संशोधन भावी प्रकृति का होगा।
ब्याज का अधिनिर्णय क्या है
धारा 34 के तहत तीन प्रकार के ब्याज देखे जा सकते हैं जो इस प्रकार हैं: –
- वाद को संस्थित करने से पहले लगाया गया ब्याज, जो आमतौर पर पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- वाद के न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) के लिए न्यायालय द्वारा लिए गए समय के लिए न्यायालय द्वारा लगाया गया अतिरिक्त ब्याज, जो कि वाद के संस्थित होने की तिथि से डिक्री की तिथि तक की अवधि है।
- अदालत के डिक्री की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए अदालत द्वारा और ब्याज भी दिया जाता है।
इन ब्याज को प्रदान करने के लिए तीनों प्रकार के ब्याज और न्यायालय के विवेक को समझना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:
एक वाद को संस्थित करने से पहले लगाया गया ब्याज
इस तरह का ब्याज या तो निर्धारित या अनिर्धारित हो सकता है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब इस प्रकार का ब्याज निर्धारित किया जाता है, तो न्यायालय के पास, भारत राज्य बनाम बी गुप्ता (चाय) लिमिटेड (1985), के मामले के निर्णय के अनुसार इस तरह के ब्याज को कम करने या बढ़ाने के लिए कम विवेक है। इसके अलावा, एक सामान्य नियम के रूप में, जहां ऐसी कोई ब्याज दर निर्धारित नहीं है, वादी को उन मामलों को छोड़कर ब्याज लगाने का कोई अधिकार नहीं है, जहां किसी व्यापारिक उपयोग के अनुसार ब्याज लगाया जाता है या जहां ब्याज का कोई वैधानिक अधिकार है। इन दिए गए अपवादों को बीएन रेलवे कंपनी लिमिटेड बनाम रतनजी (1937) और भारत संघ बनाम वाटकिंस मेयर एंड कंपनी (1966), के मामलों में निर्णयों में उजागर किया गया था। ब्याज अधिनियम, 1978, उन सभी अवधियों के लिए ब्याज का दावा करने के लिए लागू किया जा सकता है जिन पर धारा 34 लागू नहीं होती है; सीटी जेवियर बनाम पीवी जोसेफ (1995) के मामले में कानून के इसी प्रस्ताव को बरकरार रखा गया है।
वाद के अधिनिर्णयन में लगने वाले समय के लिए लगाया गया ब्याज
इस समयावधि के लिए ब्याज दर न्यायालय के विवेक का मामला है, और इस विवेकाधिकार को अनुबंध में निर्धारित ब्याज दर से भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है; यही मांगिराम बनाम धोवत राय (1886) के मामले में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, भारत संघ बनाम मुफ्फकम जाह (1995), के मामले में यह माना गया था कि अदालत को प्रतिस्पर्धी (कंपीटिंग) इक्विटी के बीच संतुलन बनाना चाहिए और वह वाद लंबित ब्याज (पेंडेंट लाइट) चार्ज करते समय मुद्रास्फीति जैसे तथ्यों का न्यायिक नोटिस भी ले सकती है। यह नियम होने के नाते, यह ध्यान रखना उचित है कि यदि प्रदान की गई ब्याज की संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुल) दर समान है, तो अदालत को इस प्रकार प्रदान की गई ब्याज की दर पर उचित ध्यान देना चाहिए। इस अवधि के लिए ब्याज प्रदान करना न्यायोचित है क्योंकि मूलधन भी कानूनी कहावत “एक्टस क्यूरिया नेमिनेम ग्रेवाबिट” में सन्निहित (एंबोडीड) है, जिसका अर्थ है कि अदालत के एक कार्य को किसी भी व्यक्ति को पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए; इस प्रकार, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह वह समय अवधि है जो अदालत द्वारा मामले को तय करने के लिए ली जाती है और इसमें डिक्री धारक की कोई गलती नहीं होती है। फिर, अदालत द्वारा डिक्री-धारक को ब्याज दिया जाता है।
सतीश सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड वी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1996), के मामले में यह माना गया था कि, एक सामान्य नियम के रूप में, इस अवधि के लिए डिक्री-धारक को ब्याज दिया जाता है; हालांकि, अगर वादी को लंबित ब्याज से वंचित करने के ठोस कारण हैं, तो अदालत दी गई अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं दे सकती है। आगे, कल्याणपुर कोल्ड स्टोरेज बनाम सोहनलाल बाजपेयी (1990) के मामले में, यह माना गया था कि अदालत न्यूनतम ब्याज देने में न्यायोचित थी, जो इस अवधि के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष था, क्योंकि वाद को संस्थित करने से पहले की अवधि के लिए ब्याज की उच्च दर ली जा रही थी। यह दिखाने के लिए यह एक आदर्श उदाहरण बन जाता है कि वाद लंबित ब्याज के लिए ब्याज की दर तय करने के लिए अदालत अपने विवेक का उपयोग कैसे कर सकती है।
डिक्री की तारीख से वसूली की तारीख तक लगाया गया ब्याज
डिक्री को प्रभावी बनाने के लिए यह ब्याज लगाया जाता है, क्योंकि यह डिक्री के निष्पादन में देरी करने से रोकने के लिए निर्णय देनदार के लिए एक निवारक (डिटरेंट) के रूप में कार्य करता है। गोरधनदास माधवजी और अन्य बनाम वाल्मजी खेतसी (1966) के मामले में यह निर्धारित किया गया कि जहां न्यायालय ने आदेश 20, नियम 11 के अनुसार धन के भुगतान को स्थगित कर दिया है या धन को किस्तों में देय कर दिया है, तो ऐसे मामले में धारा 34 लागू नहीं होगी और अधिक ब्याज दर न्यायालय द्वारा वसूल की जा सकती है। इस तरह के ब्याज को देने पर क़ानून प्रदान करता है कि एक प्रतिबंध है, जो सामान्य नियम के रूप में प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। एक अपवाद के रूप में, ऐसे मामलों में जहां एक अनुबंध है जो इस समय अवधि के लिए ब्याज की दर छह प्रतिशत से अधिक निर्धारित करता है, अनुबंध में निर्धारित ब्याज की दर अधिकतम ब्याज होगी जो अदालत लगा सकती है। यह ध्यान रखना उचित है कि यदि अदालत द्वारा पारित डिक्री ब्याज की ऐसी दर पर मौन है, तो यह माना जाएगा कि अदालत ने इस समय अवधि के लिए ब्याज देने से इनकार कर दिया है।
सीपीसी की धारा 34 की उपधारा 1 का परंतुक (प्रोवाइजो)
प्रावधान में कहा गया है कि यदि डिक्री के तहत भुगतान के बीच समय अवधि के लिए ब्याज लगाया जाता है, और यदि भुगतान एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न देयता के लिए है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% से अधिक हो सकती है; हालांकि, ब्याज की दर कभी भी अनुबंध के पक्षों द्वारा निर्धारित ब्याज दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम के. विनयचंद्रन (1989) के मामले में, अदालत ने कहा कि धारा 34 के तहत प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य से विधायिका द्वारा सभी वैधानिक अधिसूचनाओं को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 57 के तहत न्यायिक नोटिस माना जाना चाहिए। जहां अदालत न्यायिक नोटिस लेने में विफल रहती है ऐसा कोई तथ्य, एक पेटेंट दोष बन जाता है, और इस आधार पर एक समीक्षा बनाए रखी जा सकती है। उसी मामले में, यह माना गया था कि, एक सामान्य नियम के रूप में, इस तरह के अनुदान केवल एक संविदात्मक दर पर दिए जाते हैं, सिवाय इसके कि जहां न्यायालय द्वारा अपवाद बनाने के लिए पर्याप्त कारण हों। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि ऐसे अपवाद केवल दुर्लभ मामलों में ही किए जाते हैं, और अदालत को धारा 34 के तहत दी गई अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। सिंडीकेट बैंक बनाम डब्ल्यूबी सीमेंट्स लिमिटेड (1989), के मामले में भी यही कानूनी प्रस्ताव दोहराया गया था। जहां न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को यह तर्क देते हुए भी प्रमाणित किया कि, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, एक उधारकर्ता को कम ब्याज दर का लाभ इस बहाने नहीं दिया जा सकता है कि यदि उधारकर्ता डिक्री बनने के बाद फिर से भुगतान करने में विफल रहता है तो बैंक के पास कानूनी सहारा लेने का विकल्प होता है।
इस प्रावधान का एक दिलचस्प अर्थ है कि जहां पक्षकारों के बीच कोई संविदात्मक ब्याज दर निर्धारित नहीं है और लेनदेन अभी भी वाणिज्यिक है, अदालत धारा 34 के तहत प्रावधान को लागू करके 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऊपरी सीमा से आगे बढ़ सकती है; हालांकि, ऐसे मामले में, ऊपरी सीमा ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 2(B) के अनुसार होगी, जो “ब्याज की वर्तमान दर” को अलग-अलग ब्याज दर के रूप में परिभाषित करती है। ऐसे मामलों में प्रमाण का भार दावेदार पर होगा कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल की जा रही ब्याज की वर्तमान दर को साबित करे।
सीपीसी की धारा 34 से संबंधित न्यायिक घोषणाएं
वाद लंबित ब्याज
सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक बनाम मेसर्स सिबको इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (2022) के हालिया मामले में स्पष्ट किया कि वाद लंबित ब्याज अदालत का एक विवेकाधीन मामला है जो अदालत न्यायसंगत विचारों के आधार पर तय करती है। निम्नलिखित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचाराधीन मामले में ब्याज से इनकार कर दिया क्योंकि परीक्षण न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा दावा नहीं किया गया था और अपील मेमो में भी इस तरह के दावे का कोई उल्लेख नहीं था, जो इस तरह के दावे के संबंध में प्रतिवादी की गंभीरता की कमी को दर्शाता है।
मध्यस्थों द्वारा लगाया गया ब्याज
अलीमेंटा एस.ए. बनाम एन.ए.सी.एम.एफ. ऑफ इंडिया (2018) के मामले में, दो प्रमुख मुद्दों को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था। पहला मुद्दा यह है कि जहां अधिनिर्णय देने और पैसे के भुगतान के बीच की अवधि के लिए ब्याज लगाया जाता है, तो लगाया जाने वाला ब्याज केवल मूल राशि पर होगा, न कि समग्र (कंपोजिट) राशि पर, जिसमें अधिनिर्णित मूल राशि और लंबित ब्याज शामिल है जो एक अदालत द्वारा लंबित वाद में निर्णित किया गया। दूसरा मुद्दा यह है कि चूंकि मध्यस्थों (आर्बिट्रेटर्स) द्वारा अधिनिर्णय के बाद लिया जाने वाला ब्याज 11 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए सीपीसी की धारा 34 लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि धारा के तहत केवल 6 प्रतिशत तक ही ब्याज लिया जा सकता है। पहले मुद्दे के संबंध में, माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि समग्र राशि पर ब्याज लगाया जा सकता है और ब्याज अधिनियम, 1978 की धारा 3(3) या मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के किसी प्रावधान के तहत ऐसा ब्याज देने पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यदि समग्र राशि पर निष्पादन न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय के बाद का ब्याज नहीं दिया जाता है, तो वह निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री के बराबर होगा। दूसरे मुद्दे के संबंध में, यह माना गया कि सीपीसी की धारा 34, 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा प्रदान करती है, लेकिन प्रावधान अभी भी काम कर सकता है क्योंकि यह अदालत को अधिनिर्णय के बाद ब्याज देने की शक्तियां प्रदान करता है।
वाद लंबित के दौरान ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्तियों को हमेशा एक संदेहपूर्ण रूप में देखा गया था, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि कानून पूर्ण न्याय करने के लिए मामले को स्थगित करने के लिए अदालत द्वारा लिए गए समय के लिए ब्याज प्रदान करने के लिए दीवानी अदालतों को शक्तियां प्रदान करते हैं। फिर भी, एक मध्यस्थ का पद जो एक समझौते का सृजन करता है, उसे इस तरह के ब्याज को चार्ज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां समझौता स्पष्ट रूप से इसे निर्धारित नहीं करता है। न्यासी बोर्ड कलकत्ता बंदरगाह बनाम इंजीनियर्स डी स्पेस एज (1996), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 34 के तहत दीवानी अदालतों द्वारा वाद लंबित ब्याज के अनुदान (ग्रांट) के पीछे के तर्क को स्पष्ट किया कि मध्यस्थों के पास ऐसा ब्याज देने की शक्ति क्यों होनी चाहिए। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि जहां मध्यस्थ पक्षों द्वारा चुने गए विवाद समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच हैं और जहां मध्यस्थों को इस तरह के ब्याज देने की शक्तियां विस्तारित नहीं की जाती हैं, तो पक्षकार इस तरह के ब्याज के अनुदान के लिए दीवानी अदालतों में आवेदन दायर करेंगे, जो इस तरह के ब्याज के अनुदान के लिए नेतृत्व करेंगे। न्यायालय ने आगे बढ़कर स्पष्ट किया कि इस तरह का ब्याज मूल कानून का मामला नहीं है, जैसे विवाद समाधान फोरम के संदर्भ से पहले मूल राशि पर लगाया गया ब्याज; इस प्रकार, पूर्ण न्याय करने में अधिकारियों की सुविधा के लिए इन शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मध्यस्थ को इस तरह का ब्याज देने से पहले धारा 34 के सभी सिद्धांतों पर विधिवत विचार करना चाहिए।
बैंकों द्वारा वाद
ऐसे मामलों में जहां बैंक द्वारा वाद दायर किया गया है, अदालत के पास कुछ अतिरिक्त विचार हैं जिन्हें बैंक के कामकाज से संबंधित ध्यान में रखा जाता है। कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड बनाम एनवी वर्की (1987), के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा कानून का एक ही प्रस्ताव प्रकट किया गया था। जहां अदालत ने धन वाद में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देते हुए कहा कि बैंकिंग व्यवसाय इस तरह के अजीबोगरीब (पेकुलियर) मॉडल के हैं कि वे तभी चल सकते हैं जब अग्रिमों की वसूली प्रभावित हो। इसके अलावा, विजया बैंक बनाम कला ट्रेंड एक्सपोर्ट (1992), में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21A के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि जहां, बैंकों और एक इकाई के बीच एक अनुबंध में, वाद को संस्थित करने से पहले की अवधि के लिए ब्याज की दर निर्धारित की गई है, तो अदालतों के पास उसे अनदेखा करने का कोई विवेक नहीं है। इसके अलावा, इंडियन बैंक बनाम कपड़ा अंतर्देशीय एजेंसियां (1992) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां एक व्यक्ति ने बैंक के पक्ष में एक वचन पत्र निष्पादित किया है और बैंक ऐसे वचन पत्र के आधार पर वाद करता है, लंबित ब्याज के रूप में ली जाने वाली ब्याज दर, आरबीआई परिपत्रों के अनुसार ब्याज दर और प्रोनोट के उद्देश्य खंड में निर्धारित ब्याज दर होनी चाहिए, जब तक कि उसकी अवहेलना करने के प्रबल कारण न हों।
निष्कर्ष
न्यायालय द्वारा डिक्री-धारक को उस धन से वंचित होने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए ब्याज प्रदान किया जाता है, जिसके लिए वह कानूनी रूप से देनदार द्वारा हकदार है। यह मुआवजे का एक माध्यम है जिसका उपयोग पक्षकारों को उनके मूल पदों पर बहाल (रिस्टोर) करके यथास्थिति (स्टेटस क्यूओ) बनाए रखने के लिए किया जाता है। संहिता की धारा 34 को न्यायसंगत और औचित्य के प्रावधानों के अनुसार समझा जाना चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य डिक्री-धारक को वास्तविक लाभ प्रदान करना है, जो उसे उस धन से प्राप्त हो सकता था, जिसे भुगतान करने के लिए निर्णय देनदार को मजबूर किया जा रहा है। यह धारा धन की वसूली पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि ब्याज पर वाद से पहले, वाद लंबित और वाद के बाद के दौरान वसूल की जाने वाली राशि पर लगाया जाता है। पैसे के भुगतान के लिए व्यक्तिगत डिक्री के मामलों में ब्याज लगाने से संबंधित प्रावधान एक विस्तृत प्रकृति का है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या अदालत सीपीसी की धारा 34 के तहत चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकती है?
जैसा कि कालूराम बनाम चिम्निराम (1934) के मामले में आयोजित किया गया था, अदालत उस वाद के संस्थित होने की तारीख से चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकती है, जिसमें पक्षों के बीच सामान्य व्यवहार के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा था। हालांकि, ऐसे मामलों में, यह साबित करने का भार डिक्री धारक पर होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाना न्यायोचित है।
क्या सीपीसी की धारा 34 परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट) के मामलों में लागू होती है?
यह ध्यान देना उचित होगा कि परक्राम्य लिखत से संबंधित मामलों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार निपटाया जाता है, इस अधिनियम की धारा 79 में परक्राम्य लिखत से संबंधित मामलों में ब्याज लगाने का प्रावधान है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम पी कृष्णय्या (1989) के मामले में, यह माना गया था कि दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 पर भी प्रभावी होगी। तर्क यह है कि संहिता को अधिनियम के बाद लागू किया गया था। संहिता में धारा 79 जैसे प्रावधानों के अस्तित्व का संज्ञान (कॉग्निजेंट) था, लेकिन धारा 34 में किसी भी अपवाद को सम्मिलित करना विधायिका ने सचेत रूप से छोड़ा है, जो धारा 34 को धारा 79 पर प्रबल बनाने के विधायी इरादे को दर्शाता है।
संदर्भ
- The Code of Civil Procedure (Vols.1, 19th edition), 2017 by Sir Dinshaw Fardunji Mulla
- The Code of Civil Procedure (Vols.1), 2019 by M P Jain