यह लेख Rachel Sethia द्वारा लिखा गया है। यह लेख सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) के मामले का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें पृष्ठभूमि, तथ्य, मुद्दे, शामिल कानूनी पहलू और निर्णय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित ऐतिहासिक मिसालें शामिल हैं। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) का यह मामला जमानत (बेल) की अवधारणा से संबंधित है। यह “जमानत नियम है और कारागृह अपवाद है” इस मानदंड (नॉर्म) पर जोर देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटिशन) (एसएलपी) दायर की गई थी, जिसने अपना फैसला सुनाते हुए जॉन ई. ई. डी. के निबंध फ्रीडम एंड पावर को उद्धृत (कोट) किया था, जो था “स्वतंत्रता आधुनिक मनुष्य की सबसे आवश्यक आवश्यकताओं में से एक है। इसे आधुनिक सभ्यता का नाजुक फल कहा जाता है। यह सभ्य अस्तित्व का सार और आधुनिक मनुष्य की आवश्यक आवश्यकता है।” न्यायालय ने भारत में जमानत की प्रणाली की कमियों को देखा, विशेष रूप से विचाराधीन व्यक्तियों के मुद्दे के संबंध में। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के मामले में दिए गए दिशानिर्देशों के अलावा, न्यायालयों और जांच एजेंसियों के लिए कुछ प्रमुख दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।
मामले का विवरण
मामले का नाम : सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई
अपीलकर्ता : सतेंद्र कुमार अंतिल
प्रतिवादी : केंद्रीय जांच ब्यूरो
न्यायालय : सर्वोच्च न्यायालय
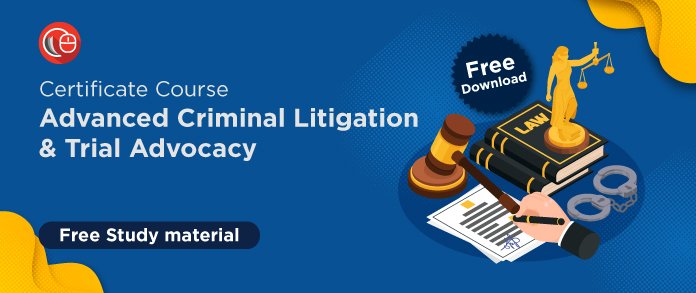
न्यायाधीशों की पीठ (बेंच) : न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश
मामले का प्रकार : विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटिशन)
फैसले की तारीख : 11 जुलाई 2022
उद्धरण (साईटेशन) : (2022) 10 एससीसी 51
सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) की पृष्ठभूमि
वर्तमान मामले से पहले 2021 में इस मामले पर दो फ़ैसले आ चुके हैं। वर्तमान मामले में आवेदक पर आरोप लगाया गया था और उसके खिलाफ़ केंद्रीय जांच विभाग (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ रेजिस्ट्रशन) (सीबीआई) ने एक प्राथमिकी (फर्स्ट इंफोर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज की थी। अभियुक्त को गिरफ़्तार किए बिना ही जांच पूरी कर ली गई और न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया गया। उल्लेखनीय यह है कि न्यायालय ने तब आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लिया और आवेदक को न्यायालय में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया। अग्रिम ज़मानत (एंटीसीपेटरी बेल) के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनने के बावजूद, अभियुक्त आवश्यक तिथि पर न्यायालय में पेश नहीं हुआ। न्यायालय ने उसकी अग्रिम ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया और उसके खिलाफ़ गैर-ज़मानती (नॉन बेलेबल) वारंट जारी किया। आखिरकार, मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। तब सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम ज़मानत पर आवेदन पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से अग्रिम ज़मानत की आवश्यकता क्यों है इस पर सवाल उठाया, क्योंकि उसे हिरासत में लिए जाने का कोई डर नहीं होना चाहिए और इसके अलावा, यह याचिकाकर्ता ही था जो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहा था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि आम तौर पर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य में, जो व्यवस्था अपनाई जाती है, वह यह है कि जांच के दौरान गिरफ्तार न किए जाने के बावजूद, अगर सीबीआई के ऐसे मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो अभियुक्त को हिरासत (कस्टडी) में भेज दिया जाता है और इसलिए, उसके सामने आने (अपीयरंस) और जमानत के लिए आवेदन करने पर उसे हिरासत में ले लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार्य योग्य पाया और मामले को स्पष्ट करने का फैसला किया। इसने कई अपराधों को वर्गीकृत किया और ऐसे मामलों के संबंध में दिशा-निर्देश (गाइडलाइन्स) निर्धारित किए, जिनमें जांच के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और संबंधित व्यक्ति को जांच के दौरान सहयोग करना चाहिए, जिसमें ऐसा करने के लिए कहे जाने पर न्यायालय के सामने पेश होना भी शामिल है।
प्रत्येक श्रेणी के लिए वर्गीकरण और दिशानिर्देश इस प्रकार हैं-
श्रेणी A: 7 वर्ष या उससे कम कारावास से दंडनीय अपराध, जो श्रेणी B और D में नहीं आते।
एक बार आरोपपत्र दाखिल हो जाने और अभिलिखित किए जाने के बाद निम्नलिखित कार्य किया जाना है:
- साधारण सम्मन जारी करें, तथा वकील के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति दें।
- जब सम्मन की तामील (सर्विस) विधिवत हो जाती है और अभियुक्त (अक्युज्ड) उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए।
- जब जमानतीय वारंट जारी हो जाता है और अभियुक्त फिर भी उपस्थित नहीं होता है, तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए।
- यदि अभियुक्त एक आवेदन दायर करता है, जिसमें वह अपेक्षित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने का वचन देता है, तो उसकी शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना, गैर-जमानती वारंट को जमानती वारंट या सम्मन में परिवर्तित किया जा सकता है।
- जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होता है, तो उसे हिरासत में लिए बिना ही जमानत आवेदन पर निर्णय किया जाना चाहिए, या जमानत आवेदन पर निर्णय होने तक उसे अंतरिम जमानत प्रदान की जानी चाहिए।
श्रेणी B: मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध।
- जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होता है, तो जमानत आवेदन पर गुण-दोष (मेरिट्स) के आधार पर निर्णय लिया जाता है।
श्रेणी C: विशेष अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराध, जिनमें जमानत के लिए कड़े प्रावधान हैं, जैसे एन.डी.पी.एस (धारा 37), पी.एम.एल.ए (धारा 45), यूएपीए (धारा 43D(5)), कंपनी अधिनियम (धारा 212(6)) आदि।
- एक बार जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, तो जमानत आवेदन पर विशेष अधिनियमों के तहत जमानत से संबंधित प्रावधानों के समुचित अनुपालन (ड्यू कंप्लायंस) के साथ, गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
श्रेणी D: विशेष अधिनियमों के अंतर्गत न आने वाले आर्थिक अपराध।
- एक बार जब अभियुक्त दी गई प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय में पेश हो जाता है, तो जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। आरोप की गंभीरता और कानून द्वारा लगाए गए दंड की गंभीरता जैसे कारकों (फैक्टर) पर उचित विचार किया जाना चाहिए।
इससे सर्वोच्च न्यायालय का 28.07.2021 का आदेश बना। 16.12.2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया-
- उस आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य जमानत की प्रक्रिया को सरल और व्यापक बनाना था, न कि उसे सीमित करना।
- आदेश की व्याख्या केवल आर्थिक अपराधों (श्रेणी D) के शामिल होने के कारण अलग नहीं होनी चाहिए, जो गैर-संज्ञेय (नॉन कॉग्निजेबल) हो सकते हैं।
- जैसा कि सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) में कहा गया है, यदि जांच के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करने का कोई कारण नहीं बनता है, तो केवल आरोप पत्र दाखिल करने से उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी।

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) के तथ्य
सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में दिशा-निर्देशों पर कुछ स्पष्टीकरण देने का निर्णय लिया तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे सीआरपीसी कहा जाएगा) की धारा 170 की गलत व्याख्या पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल होने के बाद भी जमानत आवेदनों की निरंतर आपूर्ति (सप्लाई) के मामले पर भी विचार किया।
मामले मे उठाए गए मुद्दे
क्या किसी व्यक्ति की जांच के दौरान या आरोप पत्र दाखिल होने से पहले या बाद में अनावश्यक गिरफ्तारी वैध है या नहीं?
मामले का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करके वर्तमान मामले में इस मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है। न्यायालय की व्याख्या इस प्रकार है:
परीक्षण (ट्रायल)
सीआरपीसी के तहत “परीक्षण” शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। जमानत बढ़ाने के उद्देश्य से इस शब्द को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसमें जांच का चरण (स्टेज) और उसके बाद की जाने वाली कार्यवाही शामिल हो। जांच के चरण और परीक्षण के चरण के बीच प्राथमिक विचार अलग-अलग होंगे। पहले चरण में, गहन जांच के लिए गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत की आवश्यकता हो सकती है, जबकि दूसरे चरण में परीक्षण के रूप में न्यायालय के समक्ष कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण है। जब जांच पूरी हो जाती है तो अन्य कारकों पर विचार करते हुए विस्तार के लिए अधिक अनुकूल (फेवरेबल) विचार किया जा सकता है। इसी तरह, सजा के निलंबन (सस्पेंशन) पर जमानत पर विचार करने के लिए अपील या संशोधन (रिविजन) को परीक्षण के एक पहलू के रूप में माना जाएगा।
जमानत
जमानत के उद्देश्य को विस्तार से बताने के लिए, इस शब्द को एक विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसमें जांच के चरण शामिल होंगे। जिन प्राथमिक कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वे चरण के अनुसार भिन्न होते हैं। गहन जांच के लिए, गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत आवश्यक कारक हैं, जबकि बाकी के लिए, न्यायालय के समक्ष कानूनी कार्यवाही मुकदमे का मुख्य सार है। इसलिए, जब जांच समाप्त हो जाती है, तो इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को जमानत देने के प्रति अधिक अनुकूल दृष्टिकोण रखना चाहिए।
जमानत एक निजी मुचलके (पर्सनल बॉन्ड) है जिसमें अभियुक्त की ओर से प्रतिभूति (सिक्योरिटी) शामिल होती है। जमानत न्यायालय या पुलिस या जांच संस्था (एजेंसी) के आदेश से अभियुक्त की रिहाई (रिलीज) है। अभियुक्त को इस शर्त के आधार पर रिहा किया जाता है, जहाँ वह गंभीरता से वचन देता है कि वह मुकदमे और जांच प्रक्रिया दोनों में सहयोग करेगा।
मौजूदा सिद्धांत यह है कि, जमानत नियम है और कारावस अपवाद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसे किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, आपातकाल (इमरजेंसी) के दौरान भी नहीं। गुडिकांति नरसिम्हु बनाम राज्य (1978) के मामले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने माना कि जमानत के मामले में सार्वजनिक सुरक्षा, स्वतंत्रता, न्याय और सरकारी खजाने का बोझ जैसे कारक शामिल हैं। ये कारक दर्शाते हैं कि जमानत पर एक विकसित न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडेंस) सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी अभियुक्त या दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है।

इस निर्णय में न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों की व्याख्या
धारा 41
धारा 41 में पुलिस को वारंट या न्यायाधीश के आदेश के बिना गिरफ़्तारी की अनुमति देने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। पुलिस ऐसा कर सकती है, यदि व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध किया है, या यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जो जुर्माने के साथ या उसके बिना 7 साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। पुलिस के पास यह संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार होने चाहिए कि व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। पुलिस को यह भी आश्वस्त (गारंटी) होना चाहिए कि व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए, या अपराध की विस्तृत जांच के लिए, या व्यक्ति को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, या व्यक्ति को परिस्थितियों के तथ्यों को न्यायालय में न बताने के लिए किसी को लुभाने (एंटिसिंग) से रोकने के लिए, या यदि आवश्यक होने पर उस व्यक्ति की न्यायालय में उपस्थिति की आश्वस्ति देना मुश्किल है, तो ऐसे मामले मे गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने और आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी न करने दोनों के लिए अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए।
धारा 42 (नाम और पता देने से इनकार करने पर गिरफ्तारी) को छोड़कर, किसी भी असंज्ञेय अपराध के संदिग्ध (सस्पेक्टेड) व्यक्ति को न्यायाधीश के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि धारा 41 के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने से उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जिस पर अपराध करने का संदेह है। जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय, न्यायालयों को यह अवश्य देखना चाहिए कि धारा 41 का अनुपालन किया गया है या नहीं, और यदि नहीं, तो जमानत दी जा सकती है।
धारा 41A
धारा 41A में पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बताई गई है, जब धारा 41(1) के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस को उस व्यक्ति को उपस्थिति की नोटिस जारी करना आवश्यक है जिसके खिलाफ उचित शिकायत दर्ज की गई है, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, या यह संदेह है कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय प्रकृति का है। एक बार नोटिस जारी होने के बाद, उसका अनुपालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि व्यक्ति अनुपालन करता है और ऐसा करना जारी रखता है, तो उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कि पुलिस इसे आवश्यक न समझे।
न्यायालय ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के मामले का हवाला (रेफेरंस) दिया, जिसमें उसने सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया की व्याख्या की थी। इसमें कहा गया कि पुलिस को संबंधित व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसने कोई ऐसा संज्ञेय अपराध किया हो जिसके लिए उसे जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के सात साल से कम या अधिकतम कारावास की सजा हो सकती है। गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए जब उन्हें लगे कि इसके लिए उचित आधार मौजूद हैं, जैसे कि व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकना, उसे भागने या सबूतों को नुकसान पहुंचाने से रोकना, उचित जांच करना या गवाहों को प्रभावित (इंफ्लुएंस) करने से रोकना। पुलिस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों होगी और क्या यह बिल्कुल आवश्यक होगी। उन्हें इस तरह की गिरफ्तारी के पीछे के उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। केवल अपराध करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, पुलिस को गिरफ्तारी करने और न करने के पीछे के कारणों को भी लिखना चाहिए। यदि संबंधित अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है, तो पुलिस को इन नियमों का पालन करने से छूट दी जा सकती है। अगर पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करती है और किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने के लिए पर्याप्त कारण बताने में विफल रहती है, तो वह व्यक्ति ज़मानत मांग सकता है। उसे मुकदमे के समय तक हिरासत से रिहा किया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा कि यदि पुलिस अधिकारी धारा 41 में उल्लिखित प्रक्रिया का उचित तत्परता (ड्यू डीलीजेंस) से पालन करे, तो अग्रिम जमानत की आवश्यकता कम हो जाएगी। इस न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गिरफ्तारी अनावश्यक रूप से न हो।
न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्देश (डायरेक्शंस) दिए गए:
- पुलिस अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश दिया जाना आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे आईपीसी कहा जाएगा) की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने पर कोई स्वतः गिरफ्तारी नहीं होगी। उन्हें पहले खुद को संतुष्ट करना होगा कि सीआरपीसी की धारा 41 में निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करना आवश्यक है।
- सभी पुलिस अधिकारियों को एक जांचसूची (चेकलिस्ट) दी जाएगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि व्यक्ति को कोई अन्य अपराध करने से रोकने तथा अपराध की उचित जांच के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है।
- वही जांचसूची भरी जाएगी और उसमें वह कारण और जानकारी प्रस्तुत की जाएगी जिसके कारण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- जब न्यायाधीश अभियुक्त को हिरासत में लेने का निर्णय लेते है, तो वह पुलिस द्वारा दी गई प्रतिवेदन (रिपोर्ट) पर विचार करेगा तथा अपनी संतुष्टि (सॅटीसफॅक्शन) के आधार पर हिरासत को अधिकृत करेगा।
- यदि पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय लेती है, तो मामले के प्रारंभ होने के दो सप्ताह के भीतर इस निर्णय की सूचना न्यायाधीश को दी जाएगी।
- धारा 41A के अंतर्गत अभियुक्त को मामला शुरू होने के दो सप्ताह के भीतर उपस्थिति के लिए नोटिस दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है।
- यदि पुलिस उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करने में वअसफल रहती है तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई (डिपार्टमेंटल एक्शन) की जाएगी, साथ ही वह उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) का मामला भी चलाने के लिए उत्तरदायी (लाएबल) होगा।
- यदि न्यायाधीश कारण बताए बगैर हिरासत को अधिकृत करता है, तो वह उस उच्च न्यायालय की अवमानना के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसके पास ऐसा करने का अधिकार है।
ये निर्देश भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 तथा ऐसे अपराधों पर भी लागू होंगे जिनकी निर्धारित सजा जुर्माने सहित या बिना जुर्माने के सात वर्ष से कम या अधिकतम कारावास है।
न्यायालय ने दिल्ली, झारखंड और बिहार की न्यायालयों द्वारा किए गए प्रयासों को भी स्वीकार किया और कहा कि धारा 41A के अनुपालन को लागू करने के लिए दिशा-निर्देशों का अभाव है। न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दिल्ली पुलिस की तरह कुछ दिशा-निर्देश स्थापित करने चाहिए, जिसने धारा 41 और 41A का पालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को बढ़ावा दिया और जांच संस्थाओ को अर्नेश कुमार के मामले के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें निर्दोषता के अनुमान की अवधारणा पर जोर दिया गया था। इसके अलावा, धारा 60A में कहा गया है कि गिरफ्तारी केवल सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए, और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
धारा 167
धारा 167 में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब 24 घंटे में जांच पूरी करना संभव न हो। धारा 57 के अनुसार, जब व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। यदि जांच पूरी नहीं होती है और यदि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया (प्राइमा फैसी) मामला बनता है, तो जांच अधिकारी (सब-इंस्पेक्टर से कम नहीं) निकटतम न्यायाधीश को केस डायरी प्रविष्टियों (एंट्रीज) की एक प्रति प्रस्तुत करते है और अभियुक्त को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद न्यायाधीश को अभियुक्त को 15 दिनों तक हिरासत में रखने का अधिकार है। यदि न्यायाधीश के पास मामले पर कार्यवाही शुरु करने का अधिकार क्षेत्र ना हो, तो ऐसे वक्त उस मामले को ऐसे न्यायाधीश के न्यायालय मे हस्तांतरित किया जा सकता है जिसके पास ऐसे मामले के संदर्भित अधिकार क्षेत्र है। न्यायाधीश हिरासत को 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए बढ़ा सकता है। हालांकि, हिरासत की अधिकतम अवधि 60 दिन होगी और गंभीर अपराधों के मामले में यह 90 दिन होगी। अभियुक्त को तब तक न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा जब तक वह पुलिस हिरासत में है और हिरासत को तभी बढ़ाया जा सकता है जब अभियुक्त, न्यायाधीश के सामने उपस्थित हो। द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश हिरासत का आदेश तब तक पारित नहीं कर सकते, जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा उन्हे ऐसा करने की अनुमति न दी जाए।

ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ कोई न्यायिक (जुडीशियल) मॅजिस्ट्रेट/न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, पुलिस अधिकारी को अभियुक्त और डायरी प्रविष्टियों की प्रती (कॉपी) कार्यकारी (एग्जीक्युटीव) न्यायाधीश को भेजने की आवश्यकता होती है, जो उसे लिखित रूप में कारण दर्ज कर 7 दिनों तक उसे हिरासत में रख सकता है। इन 7 दिनों में, कार्यकारी न्यायाधीश को मामले का अभिलेख उपयुक्त न्यायाधीश को भेजना आवश्यक है। इस अवधि के पूरा होने के बाद, जब तक कि कोई सक्षम न्यायिक न्यायाधीश हिरासत की अवधि को आगे नहीं बढ़ाता, तब तक अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यदि हिरासत बढ़ाई जाती है, तो हिरासत में बिताया गया प्रारंभिक समय कुल हिरासत अवधि का हिस्सा माना जाएगा। न्यायाधीश द्वारा विचारणीय किसी सम्मन मामले में, यदि जांच 6 महीने के भीतर पूरी नहीं होती है, तो न्यायाधीश को आगे की जांच को रोकना आवश्यक है, जब तक कि जांच अधिकारी न्यायाधीश को यह संतुष्टि न दे कि न्याय के हित में और विशेष कारणों के आधार पर, 6 महीने से आगे जांच जारी रखना आवश्यक है। यदि आगे की जांच को रोकने वाला ऐसा आदेश पारित किया गया है, तो सत्र (सेशन्स) न्यायाधीश को इसे रद्द करने की शक्ति है यदि वह इसे जारी रखना आवश्यक समझता है। वह जमानत और अन्य संबंधित मामलों के बारे में निर्देश भी पारित कर सकता है।
न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1978 में धारा 167(2) की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य जांच को शीघ्र पूरा करना था। प्राथमिक ध्यान शीघ्र जांच और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना था, साथ ही हाशिए पर पड़े समाज (मार्जिनलाइज्ड सोसायटी) के हितों को भी ध्यान में रखना था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जांच शीघ्रता से पूरी नहीं होती है, तो इसका परिणाम अभियुक्तों की रिहाई होगी। जैसा कि एम. रवींद्रन बनाम राजस्व निदेशालय (डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू) (2020) के मामले में कहा गया है, यह अभियुक्त का पूर्ण अधिकार है, जिसे महामारी जैसी अप्रत्याशित स्थितियों के मामले में भी निरस्त (रिपील) नहीं किया जा सकता है।
जब मामले में सजा के तौर पर सिर्फ जुर्माना है और तब यदि संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत को अधिकृत करने के लिए न्यायाधीश के सामने लाया जाता है, तो न्यायाधीश को इस प्रश्न का समाधान करना होगा कि क्या गिरफ्तारी के लिए विशिष्ट कारण दर्ज किए गए हैं या नही और यदि हां, तो प्रथम दृष्टया वे कारण प्रासंगिक होने चाहीए जिससे पुलिस अधिकारी एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि ऊपर बताई गई एक या अन्य शर्तें हिरासत करने के लिए आकर्षित होती हैं। इस सीमित सीमा (लिमिटेड एक्सटेंट) तक न्यायाधीश न्यायिक जांच करते है। न्यायालय ने उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जब कानून यह प्रावधान करता है कि धारा 167(2) के तहत बताए गए अधिकतम अवधि तक न्यायाधीश अभियुक्त को हिरासत में रखने के लिए अधिकृत कर सकते है, तो जांच संस्था द्वारा चालान दाखिल किए बिना, उस अवधि से आगे कोई भी हिरासत धोखाधड़ी होगी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी होगा।
पहले, ऐसी परिस्थितियाँ होती थीं जहाँ हिरासत की अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद आरोप लगाए जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी निश्चित अंत के लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ता था। इसे सुधारने के लिए, धारा 167(2) पेश की गई, जिसमें अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्षता (फेअरनेस) और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हिरासत के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की गई। यह धारा जांच अधिकारी द्वारा उचित साक्ष्य इकट्ठा करना अनिवार्य बनाती है, जो अनुचित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखने की रोकथाम में मदद करेगी।
न्यायालय ने राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य (2017) के मामले को भी सामने लाया, जिसमें न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया और यह उल्लेख किया कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) पर किसी भी तकनीकी मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहीए।
धारा 87
धारा 87 न्यायालय को सम्मन जारी करने के जगह पर या उसके अतिरिक्त, वारंट जारी करने का अधिकार देती है। ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ न्यायालय को सम्मन जारी करने का अधिकार है, वह अपने तर्क लिखने के बाद गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है,
- यदि युक्तिसंगत (रिजनेबल) आधारों पर न्यायालय की यह राय है कि सम्मन जारी होने से पहले या उसके बाद मे, किन्तु उसकी उपस्थिति के लिए निर्धारित की गयी अवधि से पहले, संबंधित व्यक्ति भाग गया है या सम्मन की अवहेलना करता है ।
- यदि सम्मन समय पर तामील (सर्व्ह) होने के बावजूद भी अभियुक्त निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होता है तथा इसके लिए कोई वैध कारण भी नहीं बताता है।
किसी व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने के लिए न्यायालय परिस्थिति के आधार पर सम्मन या वारंट जारी कर सकता है। धारा 87 न्यायालय को सम्मन के अतिरिक्त या उसके स्थान पर वारंट जारी करने की अनुमति देती है। वह वारंट जमानती या गैर-जमानती प्रकार का होता है।
न्यायालय ने इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य (2007) के मामले का उल्लेख किया, जिसमें न्यायालयों द्वारा वारंट जारी करने के मामले में एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, अर्थात, यह बताया गया था की मामले की शुरुआत मे अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष हाजिर कराने के लिए एक सम्मन भेजने से शुरूआत की जानी चाहीए, उसके बाद ही एक जमानती वारंट की ओर जाना चाहीए, और केवल तभी गैर-जमानती वारंट का सहारा लें जब बहुत आवश्यक हो। इस मामले मे पर्याप्त जांच और तर्क के बिना नियमित रूप से गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रथा पर नाराजगी जताई गयी है। यहा इस बात पर जोर दिया गया कि स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है, और किसी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है इस बात से सहमत होते हुए, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गैर-जमानती वारंट का इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब सार्वजनिक सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता हो।
धारा 88
धारा 88 में अभियुक्त के उपस्थिति के लिए मुचलका लेने की शक्ति दी गई है। जब कोई व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए न्यायालय को सम्मन या वारंट जारी करने का अधिकार है, वह न्यायालय में उपस्थित होता है, तो न्यायालय अधिकारी उससे, आवश्यकता पड़ने पर, उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में, जिसमें मामला सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, उस न्यायालय मे जमानतदारों के साथ या बिना जमानतदारों के, मुचलका पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
इस धारा को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने पंकज जैन बनाम भारत संघ (2018) के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या न्यायालय सीआरपीसी की धारा 88 के तहत एक मुचलका स्वीकार कर व्यक्ति को रिहा करने के लिए बाध्य था, क्योंकि उस व्यक्ति को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। यह माना गया कि यह धारा उस व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है जिसे न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। वह न्यायालय होता है जिसके पास संबंधित न्यायालय में व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विवेकाधीन शक्ति (डीस्क्रीशनरी पावर) होती है। इस धारा के तहत इस्तेमाल किया गया शब्द “कर सकता है” यह बताता है कि यह तय करना न्यायालय का विवेक है कि व्यक्ति को मुचलका पर हस्ताक्षर करना चाहिए या नहीं। धारा 88 किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो केवल गवाह हैं।
धारा 170
धारा 170 उन मामलों से संबंधित है जिन्हें पर्याप्त सबूत होने पर न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि पुलिस अधिकारी को क्या करना चाहिए, अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं या यदि अपराध कम गंभीर प्रकृति का है और वह व्यक्ति यदि जमानत पेश करता है और कार्यवाही के दौरान न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस को सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को न्यायालय को देना आवश्यक होता है और साथ ही उन्हें एक वचनबद्धता (अंडरटेकिंग) पर हस्ताक्षर करवाकर पुलीस को गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहीए, जिसकी मूल प्रती पुलिस द्वारा न्यायालय को भेजी जानी चाहिए। इसके अलावा, पुलिस को समय-समय पर किसी भी बदलाव के बारे में अभियुक्त को सूचित करना आवश्यक है। यदि मुचलका में मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय का उल्लेख है, तो इसमें अन्य सभी न्यायालयें शामिल होंगी, जिनमें न्यायाधीश मामले को सुनवाई या जांच के लिए भेज सकता है, इस शर्त पर कि मामले के पक्षों को इसके बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहीए। मुचलका की एक हस्ताक्षरित प्रती हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक को दी जाएगी और मूल प्रती को एक अभिलेख के साथ सुरक्षित रखा जाएगा जिसे मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश की न्यायालय को भेजना आवश्यक है।

इस धारा के तहत न्यायालय द्वारा जिस ऐतिहासिक मिसाल पर बहुत अधिक भरोसा किया गया, वह सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य (2021) का मामला है। उसमे धारा 170 के दायरे पर चर्चा की गई है, और यह माना गया है कि यह शक्ति न्यायालय के लिए आरक्षित है, जिसका प्रयोग वह जांच एजेंसी द्वारा अपनी जांच पूरी करने के बाद कर सकती है, जिसका अर्थ यह है कि यह न्यायालय के लिए एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है और इसमे जांच विभाग की भूमिका सीमित है। ऐसे मामलों में जहां अभियोजन पक्ष (प्रॉसीक्युशन) को अभियुक्त को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है, धारा 170 के तहत मामला न्यायाधीश के पास भेजे जाने पर अभियुक्त के गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, उसके खिलाफ जमानत याचिका दायर करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभियुक्त को केवल आरोप तय करने और मुकदमे की शुरुआत के लिए न्यायालय में भेजा जाता है। यदि न्यायालय देखता है कि वहा किसी कारागृह वापसी (रिमांड) की आवश्यकता नहीं है, तो वह धारा 88 का संदर्भ दे सकता है और मुकदमे की शुरुआत के लिए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं (फॉर्मॅलिटीज) पूरी कर सकता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां कारागृह वापसी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त व्यक्तियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, यदि न्यायालय का विचार है कि कारागृह वापसी की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि यह उन मामलों से संबंधित नहीं है, जिनमें अभियुक्त व्यक्ति पहले से ही हिरासत में हैं।
इस न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायाधीश या उसके कर्मचारियों के माध्यम से आपराधिक न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को पेश किए बिना आरोपपत्र स्वीकार करने से इनकार करना कानून के तहत उचित नहीं है। इसलिए, सभी न्यायालयों का यह कर्तव्य होगा कि जब भी पुलिस द्वारा आरोपपत्र पेश किया जाए, तो उसे आरोपपत्र में किसी चूक या आवश्यकता से संबंधित किसी भी अनुमोदन (अप्रूवल) के साथ, कर्मचारी या न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, जब पुलिस आरोपपत्र प्रस्तुत करती है, तो उसे स्वीकार करना न्यायालय का कर्तव्य है। इसी तरह, सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि यदि किसी कारण से आरोपपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उन्हें सत्र न्यायाधीश को इसके बारे में सूचित करना चाहिए, और उचित आदेश मांगना चाहिए। समीक्षा (रिव्यू) करने पर यह पाया गया कि इसके लिए प्रभारी (इनचार्ज) अधिकारी को आरोपपत्र दाखिल करने के समय प्रत्येक अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम सीबीआई (2004) का संदर्भ दिया, जिसमें न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि, क्या धारा 170, अभियुक्त को हिरासत में न लिए जाने की स्थिति में विचारणीय न्यायालय को आरोपपत्र न्यायालय के अभिलेख पर लेने से रोकती है? न्यायालय ने माना कि “हिरासत” का अर्थ विशेष रूप से न्यायालय या पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आरोपपत्र दाखिल किए जाने के समय जांच अधिकारी द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। यदि जांच अधिकारी को अभियुक्त को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं लगता है, क्योंकि वह सहयोग कर सकता है, तो अधिकारी को उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यह गलत धारणा है कि गंभीर अपराधों के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, भले ही उसकी जांच करने की आवश्यकता न हो। गिरफ्तारी केवल तभी आवश्यक है जब यह जांच के लिए महत्वपूर्ण हो और अन्य सभी कारक जैसे कि अभियुक्त भाग सकता है, वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या जब कभी आवश्यकता पड़ने पर उसके उपस्थित न होने की संभावनाहै। यदि अधिकारी को लगता है कि अभियुक्त भागने वाला नहीं है या न्यायालय के सम्मन की अनदेखी नहीं करेगा, तो उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि “हिरासत” शब्द का तात्पर्य आरोपपत्र दाखिल करते समय अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना संविधान को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ऐसा लगता है कि अभियुक्त भाग सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या कार्यवाही के दौरान सहयोग नहीं कर सकता है, तभी उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सिर्फ़ इसलिए कि कानून के तहत गिरफ़्तारी का प्रावधान है, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियुक्त को हमेशा गिरफ़्तार किया जाना चाहीए। गिरफ़्तारी करने से पहले स्पष्ट औचित्य (जस्टीफिकेशन) की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से (रुटीन मॅनर) गिरफ़्तारी करने से व्यक्ति की गरिमा और छवि को गंभीर नुकसान पहुँच सकता है। अगर ऊपर बताए गए कारक मौजूद नहीं हैं, तो न्यायालय यह समझने में विफल रहता है कि गिरफ़्तारी क्यों ज़रूरी है।
धारा 204
धारा 204 प्रक्रिया के मुद्दे से संबंधित है। संज्ञान लेने वाला न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे, तो किसी सम्मन मामले में सम्मन जारी कर सकता है, तथा किसी वारंट मामले में, वारंट या सम्मन, जो भी जरूरी हो, जारी कर सकता है, ताकि अभियुक्त को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जा सके। सम्मन या वारंट जारी करने से जुड़ी शर्त यह है कि इसे अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची दाखिल होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, जिसमें शिकायत लिखित रूप में की जाती है, उस शिकायत की एक प्रती प्रत्येक जारी किए गए सम्मन या वारंट के साथ संलग्न (अटॅच) की जानी चाहिए। यदि किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क देय है, जैसे कि न्यायालय शुल्क या कोई अन्य शुल्क, तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर, न्यायाधीश को शिकायत को खारिज करने का अधिकार मिल जाता है। इस धारा के अंतर्गत उल्लिखित कोई भी प्रावधान सीआरपीसी की धारा 87 को प्रभावित नहीं करता है।
यह एक प्रक्रियात्मक (प्रोसीजरल) प्रावधान है और स्वाभाविक रूप से इसका प्रयोग धारा 88 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए। इसलिए, वारंट जारी करना एक अपवाद है और यदि न्यायाधीश ऐसा करता है तो उसे ऐसा करने के कारण दर्ज करने होंगे।
धारा 209
धारा 209 किसी मामले को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने से संबंधित है, जब वह विशेष रूप से उसी के द्वारा विचारणीय हो। न्यायाधीश सीआरपीसी की धारा 208 या धारा 209 में उल्लिखित परिस्थितियों के आधार पर प्रक्रिया का पालन करता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय में भेजता है और अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों के अनुसार, परीक्षण (ऑब्जर्वेशन) के दौरान या उसके समापन (कंक्लूजन) तक हिरासत में रखा जा सकता है। न्यायाधीश को सत्र न्यायालय को आवश्यक अभिलेख, दस्तावेज और साक्ष्य भेजने चाहिए। इसके अलावा, इस तरह के प्रस्तुतीकरण (सबमिशन) की अधिसूचना (नोटीफिकेशन) सरकारी अभियोजक (पब्लिक प्रॉसीक्यूटर) को दी जानी चाहिए।
धारा 309
धारा 309 कार्यवाही को स्थगित करने (अद्जोर्ण ऑर पोस्टपोन) की शक्ति से संबंधित है और कहती है कि प्रत्येक जांच या परीक्षण में, कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रहेगी जब तक कि सभी गवाह न्यायालय में पेश नहीं हो जाते और उनसे जिरह (क्रॉस एग्जमीनेशन) नहीं हो जाती। यदि किसी कारण से इसे स्थगित किया जाता है, तो उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि मामला आईपीसी की धारा 376 के तहत किसी अपराध से संबंधित है, तो आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से दो महीने के भीतर परीक्षण (ट्रायल) पूरा किया जाना चाहिए। न्यायालय को संज्ञान लेने या परीक्षण शुरू होने के बाद कार्यवाही को स्थगित करने का विवेक दिया जाता है, यदि उन्हें ऐसा करना आवश्यक लगता है, और इसके लिए कारणों को लिखित रूप मे अभिलेख मे शामील किया जाना चाहिए। न्यायालय अभियुक्त को वापस हिरासत में भी भेज सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, न्यायाधीश किसी अभियुक्त को 15 दिनों से अधिक के लिए हिरासत में नहीं भेज सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि गवाह मौजूद हैं, तो उनकी जांच किए बिना कोई स्थगन या मामले को नयी तारीख नहीं दी जा सकती है, सिवाय विशेष परिस्थितियों के, जिन्हें लिखित रूप मे मामले के अभिलेख मे शामील किया जाएगा। अभियुक्त को उस पर लगाए जाने वाले दंड के विरुद्ध कारण बताने के लिए मात्र स्थगन नहीं दिया जाएगा। किसी अन्य न्यायालय में अधिवक्ता (प्लीडर) का होना भी स्थगन का आधार नहीं माना जाएगा। भले ही पक्षकार इसके लिए अनुरोध करें, स्थगन तभी दिया जाएगा जब परिस्थितियाँ पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर हों। इसके अलावा, जब कोई गवाह मौजूद हो, लेकिन उसका अधिवक्ता या पक्षकार मौजूद न हो, या जब पक्षकार या उसका अधिवक्ता गवाह की जाँच या जिरह करने के लिए तैयार न हो, भले ही वह मौजूद हो, तो न्यायालय गवाह के बयान दर्ज कर सकता है और आवश्यकतानुसार कोई भी आदेश पारित कर सकता है। इस धारा का तात्पर्य यह है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे तार्किक (लॉजीकल) अंत तक भी पहुँचना चाहिए।
हुसैनैरा खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) के मामले में, यह माना गया कि यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि अभियुक्त की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, और वह भाग नहीं सकता, तो उसे निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि, यदि परिस्थितियां भिन्न हैं और यह देखा जाता है कि अभियुक्त आपराधिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, अतीत में आपराधिक अपराध कर चुका है और उसके गायब होने की संभावना है, तो उसे जमानत के साथ रिहा किया जा सकता है, न कि निजी मुचलके के साथ। जमानत की राशि प्रासंगिक (रेलेवंट) कारकों के आधार पर तय की जानी चाहिए और मामले की प्रकृति के संबंध में पूर्व-निर्धारित (प्री डिफाइंड) नहीं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करना, किसी भी ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जो उचित नहीं है, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाकर अपनी रिहाई सुनिश्चित कर सकता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो उचित रूप से शीघ्र नहीं है, उसे उचित नहीं माना जा सकता है।

हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017) के मामले में इस प्रावधान के संबंध में कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे, जो इस प्रकार थे:
- जमानत आवेदन का निपटारा एक सप्ताह के भीतर किया जाना आवश्यक है।
- न्यायाधीश के समक्ष चल रहे मुकदमे, जिसमें अभियुक्त हिरासत में है वहा परीक्षण, को 6 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सत्र न्यायालय के समक्ष चल रहे मुकदमे के मामले में, जिसमें अभियुक्त हिरासत में है, उसे 2 वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- 5 वर्ष पुराने सभी मामलों को वर्ष के अंत तक निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- धारा 436A के अतिरिक्त, यदि किसी विचाराधीन (अंडरट्रायल) कैदी ने सजा के रूप में दी जाने वाली सजा से अधिक अवधि तक हिरासत में सजा काटी है, तो उसे निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा।
- उपरोक्त समयसीमा वार्षिक गोपनीय अहवाल (रिपोर्ट) में न्यायिक निष्पादन (जुडीशीयल परफॉर्मेंस) के मूल्यांकन (इवाल्यूएट) के लिए एक निर्देश चिन्ह (बेंचमार्क) के रूप में काम कर सकती है।
न्यायालय ने पाया कि अनावश्यक स्थगन के संबंध में कई निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि, इसके लिए अकेले न्यायालय को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि स्थगन के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। हालांकि स्थगन अपवाद हैं, लेकिन वर्तमान में यह एक नियमित रूप से होनेवाला कार्य बन गया है।
इस न्यायालय ने इस धारा का उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायालय या अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की देरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगी। यह भी माना गया कि यह प्रावधान अभियुक्त के लिए तब लाभदायी है, जब उसके जमानत आवेदन पर विचार किया जा रहा है। हिरासत में रहने के दौरान किसी भी अभियुक्त के खिलाफ लंबे समय तक मुकदमा चलाना, पुनरीक्षण (रिवीजन) या अपील करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मामले की प्रकृति यहां अप्रासंगिक है। इसलिए, न्यायालय ने माना कि उसे उम्मीद है कि धारा 309 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा, लेकिन कार्यवाही के समापन में एक अपरिहार्य (अनअवोइडेबल) और लंबी देरी जमानत अर्जी पर निर्णय लेते समय विचार करने वाला एक कारक होगी।
इस धारा के संबंध में उच्च न्यायालयों के लिए कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे, जैसे कि सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमानत आवेदनों का निपटारा एक महीने के भीतर किया जाए और जो लोग 5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं, उनके मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे सभी अधीनस्थ (सबऑर्डिनेट) न्यायालयों और प्रशासनिक (एडमिनीस्ट्रेटीव) अधिकारियों के लिए त्वरित सुनवाई और जांच के लिए योजनाएं और नये तरिके तैयार करें, जारी करें और उनकी निगरानी करें।
धारा 389
धारा 389 अपील लंबित रहने तक सजा के निलंबन (सस्पेन्शन) और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रक्रिया पर गहन विचार करती है। किसी व्यक्ति द्वारा अपील लंबित होने की स्थिति में, जिसे दोषी ठहराया गया है, अपीलीय न्यायालय को उस सजा को निलंबित करने का अधिकार है जिसके खिलाफ अपील की गई थी और कारावास के मामले में, व्यक्ति को जमानत पर या उसके अपने मुचलके पर रिहा करने का न्यायालय को अधिकार है। सरकारी अभियोजक ऐसी जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है और गंभीर अपराध के मामले में, जमानत के खिलाफ लिखित रूप में कारण बता सकते है। यदि अधिनस्थ न्यायालय में दोषसिद्धि को चुनौती दी जाती है, तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और अपीलीय न्यायालय को दी गई इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और वह पहले से ही जमानत पर बाहर रहते हुए भी उसी आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बनाता है, तो उसे दोषी ठहराने वाला न्यायालय, उसे फिर से जमानत दे सकता है, यदि संबंधित अपराध जमानत की अनुमति देता है या यदि सजा 3 साल से कम अवधि के कारावास की है। इस जमानत का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी अपील तैयार करने और प्रस्तुत करने का अवसर देना है। जमानत की अवधि के दौरान, प्रारंभिक सजा निलंबित रहती है। इसके अलावा, जब अपीलकर्ता को अंततः अपीलीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास सहित कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो अपील के दौरान उसे जमानत पर छोड़े जाने का समय उसकी सजा की अवधि की गणना करते समय घटा दिया जाएगा।
इस न्यायालय ने पाया कि इस धारा के तहत दी गई शक्ति, विचाराधीन मुकदमे के दौरान धारा 437 या धारा 439 के तहत दी गई शक्ति से भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि “निर्दोषता की धारणा” (प्रीजंप्शन ऑफ इनोसंस) और “जमानत नियम है और कारावास अपवाद है” उस अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं हो सकती है, जिसे दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा है। केवल अपील का लंबित होना ही जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अपील से निपटने में देरी के मामले में, धारा 436A से लाभ जैसे कारक उपयोग मे आते है, जो पहले से ही कारावास में बंद विचाराधीन कैदियों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने से संबंधित हैं। यदि अपील का निपटारा जल्दी नहीं किया जाता है, तो देरी से अपील करने वाले व्यक्ति को लाभ होगा। इसलिए, अन्य कारकों के साथ-साथ अपील से निपटने में देरी को भी न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है कि जमानत दी जानी चाहिए या नहीं।
अतुल त्रिपाठी बनाम यूपी राज्य (2014) के मामले में, यह माना गया कि धारा 439 और धारा 389 के तहत जमानत प्रक्रिया के बीच अंतर है। पहले वाले में सजा से पहले जमानत दी जाती है, जबकि बाद वाले में सजा सुनाई जाने के बाद जमानत दी जाती है। सजा से पहले जमानत के मामले में, जब तक कि यह एक गंभीर स्थिति न हो, अभियोजक को अभियुक्त को जमानत देने से पहले न्यायालय द्वारा केवल सूचित किया जाता है। हालांकि, सजा के बाद की जमानत के मामले में, विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियों में, सरकारी वकील को लिखित रूप में जमानत को चुनौती देने का अवसर दिया जाना चाहिए। भले ही सरकारी वकील लिखित रूप से अभियुक्त की जमानत के लिए आपत्ति बताए या ना बताए, न्यायालय को अपराध करने का तरीका, उम्र, अपराधी का आपराधिक इतिहास, अपराध की गंभीरता, उसका जनता और न्याय वितरण प्रणाली पर प्रभाव जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। इसके पीछे का इरादा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और मिलीभगत (कोल्यूजन) से मुक्त बनाना है, और यह भी सुनिश्चित करना है कि न्यायालय सजा के बाद जमानत के संबंध में अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले।
न्यायालय ने सुनील कुमार बनाम विपिन कुमार (2014) के मामले का भी उल्लेख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि धारा 389 के तहत उच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से प्रयोग किया गया है। सबसे पहले, दोनों पक्षों की आपराधिक अपील और आपराधिक पुनरीक्षण उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थे, जिसका तात्पर्य यह था कि प्रतिवादियों की सजा की पुष्टि उस कालावधी तक नहीं हुई थी। दूसरे, प्रतिवादियों पर जमानत की शर्तों का पालन करने के लिए भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि पिछले मौकों पर जमानत दिए जाने पर उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया था। अंत में, हालांकि प्रतिवादियों ने घटना के घटित होने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक वैकल्पिक (अल्टरनेटीव) स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिससे संतुष्ट होने पर उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी और सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया।
धारा 436A
धारा 436A में उस अधिकतम अवधि के बारे में चर्चा की गई है जिसके लिए किसी विचाराधीन व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति को उसके खिलाफ जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय द्वारा जमानत के साथ या उसके बिना उसके निजी मुचलके पर रिहा किया जा सकता है। सरकारी वकील (इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) को सुनने के बाद न्यायालय ऐसे व्यक्ति को अपराध की सजा की उक्त अवधि के आधे से अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है, या उसे जमानत के साथ या उसके बिना निजी मुचलके के स्थान पर जमानत पर रिहा कर सकती है। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत उक्त अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
इस प्रावधान में “करेगा” शब्द न्यायालय के लिए जमानत देने का आदेश पारित करना अनिवार्य बनाता है। जमानत के लिए आवेदन करना भी आवश्यक नहीं होगा, खासकर यदि देरी अभियुक्त के कारण नहीं हुई हो। अभियोजक की राय के आधार पर हिरासत जारी रखने का निर्णय केवल असाधारण स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। यह “निर्दोषता की धारणा” और “जमानत नियम है और कारागृह अपवाद है” पर जोर देता है। यह हमारे संविधान द्वारा आश्वासित स्वतंत्रता की अवधारणा को कायम रखता है। यह भी समझाया गया है कि ऐसी स्थिति में जिसमें अपील को अंतिम रूप देने में सामान्य से अधिक समय लग रहा है, कारावास की पूरी अवधि जिसमें परीक्षण, अपील और पुनरीक्षण का समय शामिल होगा, ऐसे वक्त उसको धारा 436A के दायरे में माना जाएगा।
भीम सिंह बनाम भारत संघ (2014) के मामले में न्यायालय ने माना कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है कि विचाराधीन कैदियों को कानून के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक कारावास में रखा जाना चाहिए या नही। कुछ न्यायिक अधिकारियों को कारावास में नियमित सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान की जा सके जो पहले ही ऊनके अप्रदह की सजा का निर्धारित समय काट चुके हैं या अपनी सजा की अधिकतम सीमा के करीब हैं। इसके बाद, उन्हें धारा 436A के तहत उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और सभी पात्र विचाराधीन कैदियों को तुरंत रिहा करना चाहिए। इन सत्रों की प्रतिवेदन उनके संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकारियों को भेजे जाएंगे। इन निर्देशों का पालन न करने पर विचाराधीन कैदियों को अनावश्यक कारावास का सामना करना पड़ेगा, जो दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने के मूल सिद्धांत के खिलाफ होगा।
धारा 437
धारा 437 में उल्लेख किया गया है कि गैर-जमानती अपराध के मामले में कब जमानत दी जा सकती है। यदि गैर-जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है या उसे उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो उसे जमानत दी जा सकती है। हालाँकि, यदि ऐसे वैध आधार मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि व्यक्ति ने आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध किया है; या यदि अपराध संज्ञेय है और व्यक्ति को पहले भी किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, तो उसे रिहा नहीं किया जा सकता है। महिलाओं, नाबालिगों (मायनर) या बीमार लोगों के मामले में अपवाद भी किए जा सकते हैं, यदि न्यायालय को इसके लिए कारण मिलते हैं। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जब तक कि यह जांच न हो जाए कि उसने गैर-जमानती अपराध किया है या नहीं। जमानत पर रिहा होने के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करना, आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में उपस्थित होना आदि जैसी शर्तें लगाई जाएंगी। न्यायालय द्वारा आवश्यक समझे जाने पर जमानत पर रिहा व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि किसी गैर-जमानती अपराध का मुकदमा 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक चलता है और अभियुक्त पूरी अवधि के दौरान हिरासत में रहा है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि न्यायाधीश इस निर्णय से असहमत न हो। न्यायालय किसी व्यक्ति को जमानत भी दे सकता है, यदि मुकदमे के बाद, लेकिन निर्णय पारित होने से पहले, यह महसूस किया जाता है कि वह दोषी नहीं है। इसके अलावा, अभियुक्त को अपील के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए जमानत मुचलका जारी करने की आवश्यकता हो सकती है और ऐसा न करने पर मुचलका जब्त किया जाता है।

न्यायालय ने प्रहलाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी, दिल्ली (2001) का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि जमानत देते समय न्यायाधीश को संबंधित सजा की गंभीरता पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर, यदि सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड की है, और यदि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो न्यायाधीश धारा 437 के प्रावधानों के अनुसार ही जमानत दे सकता है। किसी अभियुक्त के लिए सत्र न्यायालय से सीधे जमानत मांगना अधिक उचित है। इसके पीछे का तर्क यह है कि गंभीर अपराधों के संबंध में परीक्षण किए जाते हैं और उसके बाद निर्णय पारित किए जाते हैं, इसलिए जमानत आवेदनों को भी संबोधित करना तर्कसंगत है।
इशान वसंत देशमुख बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) के मामले में, यह देखा गया कि यदि संबंधित सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, और अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो न्यायाधीश को जमानत देने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि मामले को धारा 437 के तहत छूट न दी गई हो। इसलिए, केवल इसलिए कि कोई अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश को जमानत देने का अधिकार नहीं है, अपवाद की वह अपराध केवल विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय न हो। जब तक अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, न्यायाधीश जमानत दे सकता है, भले ही सजा आजीवन कारावास की हो।
धारा 439
धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालयों और सत्र न्यायालय को विशेष अधिकार प्रदान करती है। ये न्यायालय हिरासत में लिए गए किसी अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दे सकते हैं और यदि यह धारा 437(3) के तहत अपराध है, तो जमानत के लिए शर्तें तय कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते समय निचली न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कोई भी शर्त बदली या हटाई जा सकती है। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराधों के मामले में जमानत देने से पहले, जब तक कि कोई वैध कारण न हो, सरकारी अभियोजक को सूचित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि जमानत आईपीसी की धारा 376 के तहत गंभीर अपराध के लिए है, तो सरकारी अभियोजक को 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। ऐसे गंभीर अपराधों के संबंध में जमानत की सुनवाई के मामले में सूचना देने वाले या किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसके अलावा, कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और वापस हिरासत में भेजा जा सकता है।
इस बात पर जोर दिया गया कि यह शक्ति केवल धारा 437 के तहत न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णयों या सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय मामलों में ही काम आएगी। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय इस धारा के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।
न्यायालय ने धारा 437 और धारा 439 के बीच निम्नलिखित तरीके से अंतर किया। धारा 437 न्यायाधीश/मजिस्ट्रेटों को अधिकांश मामलों को सुनने का अधिकार देती है, सिवाय उन मामलों के जिनमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है और जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। धारा 437(1) महिलाओं, नाबालिगों या बीमार लोगों के लिए जमानत पर सशर्त रिहाई का प्रावधान करती है। हालाँकि यह प्रावधान अपवाद के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जमानत आवेदन का निर्धारण करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 439 जमानत आवेदन को खारिज करने वाले आदेश या विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों के मामले में लागू होती है। न्यायालयों को ऐसे कानूनों की व्याख्या इस तरह से करनी चाहिए जिससे जरूरतमंदों को लाभ हो। साथ ही उन्हे सभी आवश्यक कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
धारा 440
धारा 440 में मुचलका और कटौती (रिडक्शन) की राशि का उल्लेख है। यह कहा गया है कि इस अध्याय के तहत निष्पादित मुचलका मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद तय किया जाना चाहीए और उसकी किमत अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश द्वारा निर्धारित जमानत में कटौती का निर्देश दे सकते है।
न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुचलके की राशि उचित हो। ऐसी शर्त लगाना जिसका पालन करना असंभव हो, रिहाई के मूल उद्देश्य को विफल कर देती है। यह उल्लेख किया गया कि सीआरपीसी की धारा 436, 437, 438 और 439 की एक साथ व्याख्या की जानी चाहिए।
फिर से, न्यायालय ने हुसैन खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) का संदर्भ दिया, जिसमें यह माना गया था कि अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने के लिए लगाई जाने वाली शर्तों का निर्धारण करते समय, अपराध की प्रकृति, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का महत्व, अभियुक्त व्यक्ति की वित्तीय स्थिति, उसके पारिवारिक संबंध, चरित्र और मानसिक स्थिति, रोजगार, न्यायालय में उपस्थित होने या अभियोजन से बचने के लिए भागने से संबंधित उसका अभिलेख जैसे कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों को अभियुक्त को जमानत या व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का विवेक दिया जाता है, उन्हें इस विवेक की सीमा को समझना चाहिए और इसका उचित उपयोग करना चाहिए।
न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालयों के पास किसी व्यक्ति को जमानत देने या रिहा करने का व्यापक अधिकार है। न्यायालयों के लिए यह उचित है कि वे इस शक्ति का उपयोग करते समय अपने विवेक की सीमा को पूरी तरह समझें।
वर्तमान मामले में न्यायालय ने माना कि मौलिक पहलुओं की सुरक्षा करना न्यायालयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मौलिक पहलुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की विफलता से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता ही जो भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारत की सभी न्यायालयों, विशेषकर आपराधिक न्यायालयों को सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। न्यायालयों को आपराधिक कानून को लागू करने की आवश्यकता के साथ-साथ व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ इसके दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अर्नब मनोरंजन गोस्वानी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) के मामले में न्यायालय ने इस सिद्धांत का नेतृत्व किया। न्यायालय ने कुछ गिने चुने व्यक्तियों को ही उद्देशीत करने के कार्य के खिलाफ आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय इस तथ्य का दृढ़ विश्वासक था कि स्वतंत्रता नाजुक है और इसका उल्लंघन होने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
अपराधों की श्रेणियों (कॅटेगरी) पर स्पष्टीकरण
श्रेणी A और श्रेणी B के अपराधों के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि जमानत से संबंधित समान सामान्य सिद्धांत लागू होंगे। हालांकि, श्रेणी A के अपराधों के मामले में, न्यायालयों को ऐसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाए जा रहे अभियुक्तों के प्रति अधिक उदार होना चाहिए, जबकि श्रेणी B के अपराधों के मामले में, मामले के कानूनी सिद्धांतों और परिस्थितियों पर उचित विचार किया जाना चाहीए, जिसमे निर्णय मामले दर मामले अलग-अलग होगा।
श्रेणी C के संबंध में, जिसमें विशेष कार्य शामिल हैं, देरी के बारे में सामान्य नियम सही तौर से लागू होता है। उदाहरण के लिए, धारा 436 A विशेष कार्यों पर लागू होती है, जब तक कि उन कार्यों के लिए अलग से प्रावधान न हों। कानून, कठोर होने के बावजूद, न्याय में देरी नहीं करनी चाहिए। चूंकि ऐसे मामलों में आमतौर पर केवल कुछ गवाह होते हैं, इसलिए मुकदमे को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। न्यायालय के निर्देशों, विशेष रूप से धारा 309 का पालन करना और प्रक्रियाओं को गति देना आवश्यक है। यहां न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया (भारत संघ)बनाम के ए नजीब (2021) का संदर्भ दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि निष्पक्ष व्यवहार और उचित प्रक्रिया का पालन करने के अलावा, भारतीय संविधान न्याय और त्वरित सुनवाई भी आश्वासित करता है। यदि कोई अभियुक्त काफी समय से हिरासत में है और मुकदमे में देरी हो रही है, तो उसे आमतौर पर जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। कानून सीआरपीसी की धारा 36 के तहत विशेष न्यायालयों की मदद से प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास करता है। हालांकि, इन न्यायालयों की स्थापना में देरी इसके पूरे उद्देश्य में बाधा डालती है। इस मामले में, मुंबई क्षेत्र में विशेष न्यायालयों की स्थापना में देरी से भी न्याय में देरी हुई। न्यायालय ने मुकदमों में देरी के कारण होने वाले अन्याय पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा कि जमानत की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और मामलों को उसी के अनुसार प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्रेणी D के संबंध में न्यायालय ने सवाल उठाया कि क्या आर्थिक अपराधों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए या नहीं। इसने देखा कि चूंकि आर्थिक अपराधों में कई तरह की परिस्थितियाँ शामिल होती हैं, इसलिए इन सभी अपराधों को एक समूह में वर्गीकृत करना और फिर केवल इस वर्गीकरण के आधार पर ज़मानत से इनकार करना सही नहीं होगा। न्यायालय ने पी. चिदंबरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय (डायरेक्टरेट ऑफ एन्फोर्समेंट) (2020) का उल्लेख करते हुए उल्लेख किया कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेते समय अपराध की तीव्रता, विशेष अधिनियम का उद्देश्य, सज़ा की अवधि आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
जारी किए गए दिशा-निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए मामले का समापन किया-
- भारत सरकार जमानत देने से संबंधित प्रक्रिया और अवधारणाओं को सुचारू (स्मूथ) बनाने के लिए जमानत से संबंधित एक अलग कानून लाने पर विचार कर सकती है।
- जांच विभाग का यह कर्तव्य है कि वे धारा 41 और धारा 41A के प्रावधानों का पालन करें और अर्नेश कुमार फैसले के तहत दिए गए निर्देशों का पालन करें। उनकी ओर से किसी भी तरह की गैर-अनुपालन की प्रतिवेदन को उच्च और उचित प्राधिकारी (अथॉरीटी) को दी जाएगी।
- न्यायालयों को धारा 41 और धारा 41A का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। अनुपालन न करने पर अभियुक्त को जमानत दी जाएगी।
- सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश धारा 41 और धारा 41A के कार्यान्वयन (एस्टॅब्लीशमेंट) के लिए मानक (स्टँडर्ड) प्रक्रियाएं स्थापित करेंगे।
- धारा 88, धारा 170, धारा 204 और धारा 209 के तहत आवेदनों पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर नहीं दिया जाएगा।
- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में उल्लिखित आदेश का कड़ाई (स्ट्रीक्ट) से अनुपालन आवश्यक है।
- राज्य और केंद्र सरकारें विशेष न्यायालयों की स्थापना के संबंध में न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगी। उच्च न्यायालय को राज्य सरकार के परामर्श (कन्सल्टेशन) से विशेष न्यायालयों की आवश्यकता के संबंध में कार्य करना चाहिए तथा पीठासीन अधिकारियों की रिक्तियों (वॅकंसीज) को शीघ्रता से भरा जाना चाहिए।
- ऐसे विचाराधीन कैदी जो जमानत की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते, उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित (मार्क) किया जाना चाहिए तथा उनकी रिहाई के लिए धारा 440 के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- जमानत पर जोर देते समय धारा 440 के अधिदेश (मँडेट) को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- भीम सिंह के मामले में दिए गए निर्देशों के समान, उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका को सीआरपीसी की धारा 436 A का अनुपालन करने के लिए मूल्यांकन (असेसमेंट) करना होगा, जिसके बाद आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे।
- ज़मानत आवेदनों का निपटारा दो सप्ताह के भीतर किया जाना आवश्यक है, सिवाय इसके कि प्रावधान में इसके विपरीत कुछ उल्लेख किया गया हो। अग्रिम ज़मानत आवेदनों का निपटारा छह सप्ताह के भीतर किया जाना चाहीए, सिवाय इसके कि ऐसा आदेश पारित न हो इसलिये कोई आवेदन न किया गया हो।
- राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को चार महीने की अवधि के भीतर स्थिति प्रतिवेदन /शपथपत्र दाखिल करना आवश्यक है।
सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) का आलोचनात्मक विश्लेषण (क्रिटिकल अनालिसीस) xx
यह निर्णय उन व्यक्तियों की लंबे समय तक और अवांछित (अनवॉन्टेड) हिरासत से संबंधित है जो अपनी अपील की सुनवाई के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह उन मामलों में जमानत की अवधारणा को स्पष्ट करता है जिनमें न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल करने के समय अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता है।
न्यायपालिका के निचले स्तर पर आम तौर पर अभियुक्त को जमानत देने में अनिच्छा होती है, जिसके कारण कई बार निर्दोष व्यक्ति को लंबे समय तक कारावास का सामना करना पड़ता है। जब अपीलों के निपटारे में बहुत लंबा समय लग जाता है, तो यह जोखिम पैदा होता है कि व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलने से पहले ही पूरी सजा काट लेगा। अक्सर इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार, जमानत से इनकार करने का एकमात्र वैध औचित्य (जस्टिफिकेशन) तब है जब जांच की अखंडता की रक्षा के लिए अभियुक्त को हिरासत में लेना आवश्यक हो। वर्तमान में पुलिस द्वारा की जा रही गलती सभी संदिग्धों को गिरफ्तार करने की प्रवृत्ति है, जो सात साल से कम कारावास की सजा वाले कानूनों के संबंध में आवश्यक नहीं है।
इस निर्णय के पीछे सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य जमानत की अवधारणा और दायरे को व्यापक (वाईड) बनाना तथा जमानत के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली सभी शंकाओं का समाधान करना था। यह निर्णय मानवीय स्वतंत्रता तथा आपराधिक न्यायालयों और जांच विभागो के संवैधानिक मूल्यों और लोकाचार (इथोज) की रक्षा करने के कर्तव्य को बनाए रखने का प्रयास करता है। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद, अभियुक्त को हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता।
निर्दोषता की अवधारणा पर जोर देना आवश्यक है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से हिरासत में रखना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और कानून के विरुद्ध है। इस मामले पर विचार करते हुए, न्यायालय ने उल्लेख किया कि हमारे देश के कारावास विचाराधीन कैदियों से भरी पड़ी हैं। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि दो-तिहाई से अधिक कैदी विचाराधीन हैं और उनमें से उन अपराधों के अभियुक्त हैं जिनकी सजा सात वर्ष से कम है और उन्हें गिरफ्तार करने की भी आवश्यकता नहीं है।
न्यायालय द्वारा पाया गया एक प्रमुख बिंदु यह था कि गरीबों को जमानत देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जमानत की राशि अधिक होती है और कभी-कभी जमानतदारों की आवश्यकता होती है, खासकर जब वे पूर्व-परीक्षण (पूर्व परीक्षण) हिरासत में होते हैं। न्यायालय ने जमानत आवेदनों को परीक्षण कार्यवाही से अलग करने का भी प्रयास किया है और कहा है कि जमानत के लिए एक अलग कानून होना चाहिए।
न्यायालय ने निरंतर हिरासत की अन्यायपूर्ण प्रकृति जिसके कारण अभियुक्त के बरी होने के मुद्दे पर बहुत जोर दिया है, और संविधान को सबसे उपर रखने और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए न्यायालयों के कर्तव्य पर भी जोर दिया गया। यहां न्यायालय का एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि न्यायालय को न्याय के उद्देश्यों को पूरा करते हुए कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है और इन्हे निर्णय पारित करते समय सावधानी बरतने का अनुरोध किया।
इस निर्णय के आलोक (व्यू) में सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखा जाना चाहीए और व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नही किया जाना चाहीए। न्यायालय ने जमानत के लिए एक अलग कानून की वकालत की है जो दर्शाती है कि जमानत देने में स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण न केवल निर्दोषता के अनुमान के महत्व को उजागर (हायलाइट) करता है बल्कि जमानत हासिल करने में अभियुक्तों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता की आवश्यकता को भी उजागर करता है।

निष्कर्ष
कानूनी व्यवस्था के आपराधिक पक्ष के वर्तमान परिदृश्य (सिनेरीयो) को देखते हुए जमानत की अवधारणा को स्पष्ट करना अत्यधिक आवश्यक था। “जमानत नियम है और कारावास अपवाद है” वास्तव में व्यवहार में नहीं है, जिसके कारण कई लोग कारावास में बंद हो जाते हैं और ऐसे अपराध के लिए सजा काटते हैं जिसके वे दोषी नहीं होते हैं, जिससे भारतीय संविधान के तहत उनके कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। जमानत प्राप्त करना आसान प्रक्रिया नहीं है, इसमें जमानत मुचलका, जमानतदार (श्यूरिटीज) शामिल होते हैं जो इसे एक लंबी प्रक्रिया बनाते है। कारागृहो में भीड़भाड़ हो जाती है और मामलों की संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि जमानत आवेदन आमतौर पर लंबे समय तक अनसुने रह जाते हैं। भारत में जमानत की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, जिसे समान शर्तें, उचित जमानत राशि निर्धारित करके प्राप्त किया जा सकता है जिसे लोग वहन (अफोर्ड) कर सकते हैं और जो प्रक्रिया को आसान बनाता है। न्यायालय ने वर्तमान परिदृश्य को पलटने का प्रयास किया है जो कि “कारागृह नियम है और जमानत अपवाद है”, लेकिन बेहतर समाधान की हमेशा आवश्यकता होती है, अन्यथा न्याय केवल कागजों पर ही रह जाएगा।
संदर्भ







