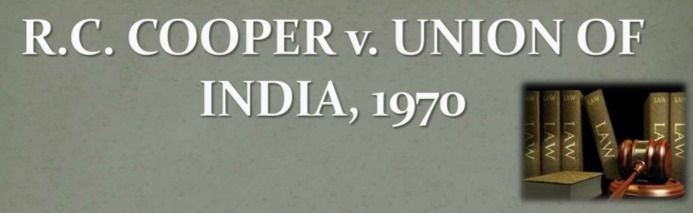यह लेख एमिटी यूनिवर्सिटी, कोलकाता से बीबीए एलएलबी (ऑनर्स) के छात्र रौनक चतुर्वेदी ने लिखा है। इस लेख में आर सी कूपर मामले के तथ्य, मुद्दे, तर्क और प्रलय के बारे में बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar ने किया है।
Table of Contents
परिचय (इंट्रोडक्शन)
“समाजवाद (सोशलिज्म)” यह वह विशेष शब्द है जो इस मामले में हुई हर चीज का कारण था। भारत में समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक उपलब्धि के कारण ही इस लेख के माध्यम से जो कुछ भी बताया जा रहा है, वह हुआ। आइए पहले इस विशेष मामले से संबंधित कुछ बुनियादी (बेसिक्स) बातों को समझते हैं।
समकक्ष प्रशस्ति पत्र (इक्विवालेंट सायटेशन)- एआईआर 1970 एससी 564; 1970 एससीआर (3) 530
याचिकाकर्ता का नाम (नेम ऑफ़ द पेटीशनर)- रुस्तम कावासजी कूपर/आर. सी कूपर
प्रतिवादी का नाम (नेम ऑफ़ द डिफेंडांट)- भारत संघ (यूनियन ऑफ इंडिया)
केस का प्रकार (टाईप ऑफ़ केस)- 1969 की रिट याचिका (पेटिशन) संख्या 298 और 300, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत के संविधान (इंडियन कंस्टीट्यूशन) के अनुच्छेद (आर्टिकल) 32 के तहत दायर (फाईल) की गई।
निर्णय की तिथि (डेट ऑफ जजमेंट)- 10/02/1970
फैसले के लेखक (ऑथर्स ऑफ़ द जजमेंट)-
बहुमत का फैसला (मेजॉरिटी जजमेंट), जो 11 में से 10 न्यायाधीशों (जजेस) द्वारा दिया गया था, न्यायमूर्ति जे सी शाह ने अपने लिए और अन्य 9 न्यायाधीशों की ओर से जो बहुमत के फैसले के लिए थे उनकी राय से बहुमत का मसौदा तैयार किया था। असहमति के आदेश (डेसेंटिंग ऑर्डर) का मसौदा न्यायमूर्ति ए एन रे ने तैयार किया था। इस प्रकार, इस विशेष मामले (पर्टिकुलर केस) में निर्णय 10:1 बहुमत से पारित किया गया था।
न्यायाधीशों के नाम (नेम्स ऑफ़ द जजेस)
इस ऐतिहासिक निर्णय (लैंडमार्क जजमेंट) में शामिल होने वाले न्यायाधीश इस प्रकार हैं-
- जस्टिस जेसी शाह।
- न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी।
- न्यायमूर्ति जेएम शेलत।
- न्यायमूर्ति विशिष्ट भार्गव।
- न्यायमूर्ति जी.के. मिटर।
- न्यायमूर्ति सी.ए. वैद्यलिंगम।
- न्यायमूर्ति के.एस. बचाव।
- न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर।
- न्यायमूर्ति ए.एन. रे।
- न्यायमूर्ति जगमोहन पी. रेड्डी।
- न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ।
मामले के तथ्य (फैक्ट्स ऑफ़ द केस)
मामले के तथ्यों को समझने के लिए हमें भारत के इतिहास को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। भारत के पहले प्रधान मंत्री, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद को देश की प्रगति के अनुकूल विकास (बेस्ट डेवलपमेंट) का सबसे अच्छा मॉडल मानते थे। वास्तव में, जिस प्रकार के समाजवाद में उनका विश्वास था, उसे फैबियन समाजवाद कहा गया। इसका अर्थ था कि राष्ट्र की बेहतर प्रगति, उसके नागरिकों की भलाई और विकास के लिए, कुछ उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण (स्टेट कंट्रोल) रखना आवश्यक था, जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता था।
स्वतंत्रता के बाद, राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कई क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण (नेशनालाइज्ड) किया गया। उदाहरण के लिए, परिवहन उपक्रम (ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग), बीमा क्षेत्र (इंशुरंस सेक्टर) और बिजली (इलेक्ट्रिसिटी) को पूरी तरह से राज्य का एकाधिकार (मोनोपली) प्रदान किया गया था। हालाँकि, 1960 के दशक में तेल और रिफाइनरियों का राष्ट्रीयकरण कुछ समय बाद किया गया था।
वर्तमान मामले में, जिसे बैंक राष्ट्रीयकरण मामले (नेशनालाइजेश ऑफ़ बैंकिंग) के रूप में जाना जाता है, बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव वास्तव में भारत के लिए बहुत नया नहीं था। वास्तव में, वर्ष 1948 में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए आय सी सी) द्वारा बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप (एक्टिवली) से बहस की गई थी। भारत के पहले वित्त मंत्री (फाइनेंस मिनिस्टर) आर.के. षणमुगम शेट्टी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने कुछ राजनीतिक कारणों से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। हालाँकि, बहुत जल्द, वर्ष 1955 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम (एक्ट) के तहत राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इसकी 7 सहायक (सब्सिडियरी) कंपनियों को भी सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था। इसलिए, हम इस बिंदु (पॉइंट) से देख सकते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र का आंशिक राष्ट्रीयकरण (पार्शियल नेशनालाईजेशम) पहले ही शुरू हो चुका था।
राष्ट्रीयकरण की इस प्रक्रिया (प्रोसेस) में भारतीय रिजर्व बैंक की भी भूमिका बहुत उल्लेखनीय (नोटेवर्थी) है। रिज़र्व बैंक ने धीरे-धीरे भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग संस्थानों (कमर्शियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन) की संख्या को 1951 में 566 से घटाकर 1969 के अंत तक केवल 89 कर दिया।
अब, हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, सरकार में कुछ ऐसे नेता थे जो बैंकों के इस राष्ट्रीयकरण के विरोध में थे। तत्कालीन वित्त मंत्री (देन फाइनेंस मिनिस्टर) मोरारजी देसाई अपने पिता के आदर्शों का पालन करते हुए इंदिरा गांधी द्वारा भारत में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। देसाई उस समय उप प्रधानमंत्री भी (डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर) थे। श्री देसाई का मुख्य तर्क (आर्गुमेंट) यह था कि इन बैंकों को जो मुआवजे (कंपनसेशन) का भुगतान किया जाना था, जो कि 85 करोड़ रुपये था, इसका सीधा उपयोग देश की अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) को गति देने के लिए किया जा सकता है। एक और तर्क जो श्री देसाई ने सामने रखा था, वह यह था कि देश के बैंकिंग कानूनों (बैंकिंग लॉज) में संशोधन (अमेंडमेंट) करके केवल बैंकों को नियंत्रित करके ऋण (क्रेडिट) को सामाजिक क्षेत्रों (सोशल सेक्टर) की ओर मोड़ा जा सकता है।
दोनों के बीच मतभेद इतने गंभीर हो गए कि 17 जुलाई 1969 को मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से बर्खास्त (डिस्मिसल) कर दिया गया। अगले ही दिन उन्होंने अपनी इच्छा से भारत के उप प्रधान मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
इसी के बीच भारत के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति (देन एक्टिंग प्रेसिडेंट) न्यायमूर्ति (जस्टिस) एम. हिदायतुल्ला ने संसद (पार्लियामेंट) का मानसून सत्र (सेशन) शुरू होने से ठीक दो दिन पहले एक अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) जारी किया था। अध्यादेश का नाम ‘बैंकिंग कंपनी {संपत्ति का अधिग्रहण (एक्विजिशन) और हस्तांतरण (ट्रांसफर)} अध्यादेश 1969’ था। आइए अब सबसे पहले यह समझें कि यह अध्यादेश क्या था? अध्यादेश की विशेषताओं को नीचे दिए गए मुद्दों नुसार सूचीबद्ध (लिस्टेड) किया जा सकता है:
- अध्यादेश में भारत के 14 बैंकों को सूचीबद्ध किया गया था जिनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था।
- इन 14 बैंकों को उनके पास जमा राशि (अमाउंट) के आधार पर चुना गया था। यानी इन सभी बैंकों के पास 50 करोड़ से अधिक की जमा राशि थी, जिसे राष्ट्रीयकरण के लिए चुनने की कसौटी (क्राइटेरिया) के रूप में लिया गया था।
- इन 14 बैंकों के सभी निदेशकों (डायरेक्टर्स) को अपने कार्यालय खाली करने को कहा गया था। हालांकि, निदेशकों के अलावा, बाकी कर्मचारियों को भारत सरकार के तहत अपनी नौकरी जारी रखने की अनुमति दी गई थी।
- अध्यादेश की दूसरी अनुसूची (शेड्यूल) सबसे असंवैधानिक हिस्सा (अन कॉन्स्टिट्यूशनल) थी। इसमें उस मुआवजे के बारे में बात की गई थी जो सरकार के अधिकार के नीचे किए जा रही बैंकों को भुगतान किया जाना था। अध्यादेश में पीड़ित बैंकों (अग्रीव्ड) को मुआवजा प्रदान करने के दो प्रमुख तरीकों का उल्लेख किया गया है-
- जब समझौता (अग्रीमेंट) हुआ था- जब मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि एक समझौते के माध्यम से तय की जा रही थी, तो यह ठीक था।
- जब कोई समझौता नहीं किया जा सकता था- जब कोई समझौता नहीं हो रहा था, तो विवाद मामले (डिस्प्यूट मैटर) को एक समझौते तक पहुंचने में विफलता की तारीख से तीन महीने के भीतर ट्रिब्यूनल को भेजा जाना चाहिए था। ट्रिब्यूनल द्वारा जो भी मुआवजे की राशि तय की जानी थी, उसे सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के रूप में दिया जाना था। ये सरकारी प्रतिभूतियां तुरंत प्रतिदेय (रिडिमेब्ल) नहीं थीं, लेकिन, जारी किए जाने के 10 साल बाद प्रतीदेय की जा सकती थी।
- अध्यादेश पारित होने के दो दिन बाद, जब संसद ने अपना मानसून सत्र शुरू किया, तब इंदिरा गांधी सरकार ने तुरंत ‘बैंकिंग कंपनी (संपत्ति का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1969’ तैयार किया और हर प्रावधान अध्यादेश के समान ही था।
अध्यादेश की घोषणा (प्रोमुलगेशन) की खबर के बाद श्री कूपर पहुंचे, जो न केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक (थीं डायरेक्टर) थे, बल्कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड और बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड में उनके शेयर भी थे, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया था कि अध्यादेश के प्रख्यापन से उनके मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) का उल्लंघन (वायोलेटेड) किया गया था।
रिट याचिका 21 जुलाई, 1969 को दायर की गई थी और अंतरिम आवेदन (इंटरीम एप्लिकेशन) पर 22 जुलाई, 1969 को सुनवाई (हीयरिंग) हुई थी। अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के बाद, न्यायालय ने निदेशकों को उनके कार्यालयों से तुरंत खाली होने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा (इंजंक्शन ऑर्डर) दी।
उठाए गए मुद्दे (इश्यूज रेज्ड)
श्री कूपर ने अपने अधिवक्ता (एड्वोकेट) श्री पालखीवाला के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दे उठाए थे, जो इस प्रकार हैं-
- क्या एक शेयरधारक (शेयरहोल्डर) अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एक रिट याचिका दायर कर सकता है, जब वह कंपनी जिसमें वह एक शेयरधारक है, सरकार द्वारा अधिग्रहित (एक्वायर) किया जाता है?
- प्रश्नगत अध्यादेश (ऑर्डिनेंस इन क्वेश्चन) ठीक से बनाया गया था या नहीं?
- अधिनियम तैयार करना संसद के अधिकार क्षेत्र में था या नहीं?
- क्या आक्षेपित अधिनियम (इंपुग्नेड एक्ट) भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन था या नहीं?
- मुआवजे का निर्धारण (एसेर्टेनिंग) करने का तरीका वैध (वेलिड) था या नहीं?
प्रस्तुत किए गए तर्क (आर्गुमेंट्स सबमिटेड)
याचिकाकर्ता (पेटिशनर):
- श्री पालखीवाला द्वारा याचिका की रख-रखाव (मेंटेनाबीलिटी) के संबंध में प्रस्तुत पहला तर्क यह था कि याचिका को बनाए रखने योग्य था, इस बहाने कि श्री कूपर द्वारा भारत के नागरिक (सिटिज़न ऑफ़ इंडिया) के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता (इंडिविजुअल कपेसिटी) में याचिका दायर की जा रही थी, न कि उनके कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में। चूंकि एक कंपनी भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के दायरे में नागरिक नहीं है, इसलिए, यह संविधान के तहत किसी भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकती है, जिसके नागरिक होने के आधार पर श्री कूपर पात्र थे।
- अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी भी अध्यादेश को पारित (पास) करने का अधिकार है, यदि उसे लगता है कि इसकी परम आवश्यकता (एब्सोल्यूट नेसेसिटी) है और जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हैं। इस तर्क के आधार पर, हम देख सकते हैं कि संसद के मानसून सत्र से ठीक दो दिन पहले अध्यादेश जारी किया गया था, इसलिए इसे लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, इस प्रावधान के उल्लंघन में, सुप्रीम कोर्ट को इसे रद्द करने का अधिकार दिया गया था।
- तीसरा तर्क अधिनियम पारित करने के लिए संसद की योग्यता के संबंध में था। यह कहा गया था कि सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां शामिल हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमा का सीमांकन (डिमार्केट) करती हैं। संघ सूची (यूनियन लिस्ट) में ऐसी प्रविष्टियाँ (एंट्रीज) थीं जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार था, राज्य सूची में ऐसी प्रविष्टियाँ थीं जिन पर केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था और अंत में, समवर्ती सूची (कंक्योरंट लिस्ट) में ऐसी प्रविष्टियाँ थीं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विरोध (डॉक्ट्रिन ऑफ़ रिपग्नुंसी) के सिद्धांत के अधीन कानून बना सकती थीं। इस प्रकार, तर्क में कहा गया कि केंद्र सरकार केवल ‘बैंकिंग’ पर कानून बनाने की हकदार थी, जैसा कि 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 (बी) के तहत परिभाषित किया गया था, क्योंकि संघ सूची की प्रविष्टि (एंट्री) 45 ने इसे ऐसा करने का अधिकार दिया था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया था कि समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के आधार पर, विधायिका (लेजिस्लेचर) को केवल संघ सूची में प्रविष्टि 45 को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार, इन तर्कों के आधार पर, यह कहा गया कि संसद को आक्षेपित अधिनियम को पारित करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था।
- उस समय, संपत्ति के अधिकार (राइट टु प्रॉपर्टी) को अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत एक मौलिक अधिकार माना जाता था, जिसे बाद में केशवानंद भारती के मामले के निर्णय के बाद हटा दिया गया था। हालाँकि, जब वर्तमान मामला स्थापित किया गया था, तो अधिकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी और इसलिए यह कहा गया था कि यह अनुच्छेद 19 (1) (g) अनुच्छेद 31 (2) (पूरा लेख अब निरस्त कर दिया गया है) का उल्लंघन करता है जो संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण (कंप्लूसरी एक्विजिशन ऑफ़ प्रॉपर्टी) से संबंधित है।
- अंत में और कम से कम, इस पूरे अधिनियम की अकिलीज़ एड़ी मुआवजे का प्रावधान था, जिसे पूरी तरह से ‘कठोर’ और अत्यंत तर्कहीन (रेशनल) और अतार्किक (इलॉजिकल) होने का तर्क दिया गया था। मुआवजा, जो नकद (कैश) में भुगतान नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों में, जो बदले में 10 वर्षों के बाद देय थे, जनता को परेशान करने के उद्देश्य से और साथ ही, सरकार एक अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से अपने दृष्टिकोण में पूरी तरह से पक्षपाती था।
प्रतिवादी (रेस्पोंडेंट):
- प्रतिवादी का पहला तर्क रिट याचिका की स्थिरता के संबंध में था और उसने कहा कि यह याचिका अनुरक्षणीय (मेंटेनेबल) नहीं थी, क्योंकि इसे एक कंपनी के नाम पर अधिकारों का दावा करने के लिए दायर किया जा रहा था, जैसा कि हमने देखा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नागरिक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
- अगला तर्क अध्यादेश को प्रख्यापित (प्रोमुलगेट) करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में प्रश्न के संबंध में था। यह तर्क दिया गया था कि अध्यादेश को प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूरी तरह से व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) प्रकृति की थी, क्योंकि ‘अगर उन्हें लगा’ इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और साथ ही, वह अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थे। इस प्रकार, अध्यादेश की अमान्यता (इनवैलिडिटी) के तर्क की निंदा (कंडेमड़) की गई।
- संसद की क्षमता के संबंध में दूसरा तर्क यह था कि न्यायालय को यह समझना चाहिए कि समतावाद (इगल्टिनियारिज्म) के सिद्धांतों के साथ एक समाजवादी समाज को प्राप्त करना और जहां कोई असमानता मौजूद न हो यह राज्य का दायित्व था। इस परिभाषा पर विचार करते हुए, अगला तर्क यह था कि न्यायालय को ‘बैंकिंग’ शब्द की व्यापक (वाइडस्ट) रूप से व्याख्या करनी चाहिए, ताकि प्रतिवादी द्वारा शामिल की जा सकने वाली सभी गतिविधियों (एक्टिविटीज) को इसमें शामिल किया जा सके।
- चौथा तर्क एक दूसरे से मौलिक अधिकारों की पारस्परिक विशिष्टता (म्युचल एक्सक्लूसिविटी) के संबंध में था, जैसा कि ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में आयोजित किया गया था और कहा कि अधिनियम अनुच्छेद 19 (1) (g) का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 31 के दायरे में आता है।
प्रलय (जजमेंट)
2 फरवरी, 1970 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10:1 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया गया। सिवाय जस्टिस ए. एन. रे, अन्य न्यायाधीशों ने निम्नलिखित निर्णय दिया कि एक शेयरधारक अपनी कंपनी के नाम पर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का हकदार नहीं था, जब तक कि कार्रवाई जिसकी शिकायत की जा रही थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार भी उल्लंघन नई करता।
निर्णय का औचित्य (रेशो डिसिडेंडी)
वर्तमान मामले में न्यायालय के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं (द मेजर फाइंडिंग ऑफ़ द कोर्ट इन द प्रेजेंट केस आर एज फॉलोज)
- इस मामले का प्रमुख योगदान ‘म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी थ्योरी’ को खत्म करना था, जो इस मामले के होने तक 20 साल तक अभ्यास (प्रैक्टिस) किया गया था, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में कोर्ट ने कहा कि सिर्फ तकनीकी (टेक्नीकैलिटिज) के आधार पर, वह एक याचिका को खारिज नहीं कर सकता है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि एक विधायी कार्रवाई भी कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, इसका मतलब यह नहीं था कि न्यायालय के पास कंपनी के शेयरधारक के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। न्यायालय ने ‘वस्तु’ परीक्षण (ऑब्जेक्ट टेस्ट) को भी रद्द कर दिया और ‘प्रभाव’ परीक्षण निर्धारित किया। प्रभाव परीक्षण अब किसी विशेष विधायी अधिनियम के प्रभाव पर गौर करेगा, न कि उस उद्देश्य को देखने के लिए जिसके साथ इसे तैयार किया गया था। इस प्रकार, यदि विधायिका का कोई अधिनियम, दूरस्थ स्तर पर भी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे निरस्त (स्ट्रक) किया जा सकता था।
- जहां तक अध्यादेश को ठीक से प्रख्यापित किया गया था या नहीं, इस पर न्यायालय ने कहा कि चूंकि अध्यादेश को पहले ही एक अधिनियम में बदल दिया गया था, इसलिए न्यायालय के लिए उस पर चर्चा करना अनावश्यक था। कोर्ट ने कहा कि यह शिक्षाविदों (एकेडमिशियन) के लिए विचार करने का प्रश्न बन गया है, लेकिन वर्तमान मामले के लिए नहीं।
- जहां तक बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण के लिए संसद की क्षमता के बारे में तर्कों का संबंध था, अदालत ने बहुत दिलचस्प (इंटरेस्टिंग) तरीके से याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों के तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति शब्द में सभी अधिकार, देनदारियां (लायबिलिटी), संपत्ति आदि शामिल हैं, जो संपत्ति से जुड़े थे। किसी भी बैंकिंग कंपनी को हासिल करने की संसद की शक्ति संसद की एक स्वतंत्र शक्ति थी और इसके लिए सूची II और सूची III के तहत पहले अलग कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी।
- कोर्ट ने अधिनियम को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 31 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया, क्योंकि अनुच्छेद 31 में अर्जित संपत्ति (एक्वायर्ड) के मुआवजे के बारे में बात की गई थी। अब, ‘मुआवजा’ शब्द का अर्थ उस व्यक्ति को पूर्ण क्षतिपूर्ति है, जिसकी संपत्ति अर्जित की जा रही थी। चूंकि यह अधिनियम के उद्देश्यों से स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि समान क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा रही थी और साथ ही, पृथक्करणीयता के परीक्षण को लागू करने के बाद, क्योंकि अधिनियम स्वतंत्र रूप से प्रश्न में भाग के बिना अकेले खड़े होने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए यह उत्तरदायी था मारा जाना है।
- हालाँकि, न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(g) के तर्क के लिए कहा कि यह अधिनियम अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि राज्य को किसी भी व्यवसाय पर आंशिक या पूरी तरह से एकाधिकार करने का पूरा अधिकार है। को महसूस किया।
- हालांकि, कोर्ट ने पाया कि अधिनियम अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन था। यह निम्नलिखित कारणों के आधार पर आयोजित किया गया था कि संबंधित अधिनियम ने देश के भीतर बैंकिंग गतिविधियों को करने वाले 14 बैंकों को प्रतिबंधित कर दिया था, हालांकि, विदेशी सहित अन्य बैंक बैंकों को ऐसा करने से नहीं रोका गया। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को ‘भेदभाव का खुलकर अभ्यास’ करने वाला माना और इस प्रकार, इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया।
न्यायमूर्ति ए.एन. राय एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने असहमतिपूर्ण राय दी। उन्होंने निम्नलिखित बिंदु दिए (जस्टिस ए एन रे इज द ओनली जज हू गेव द डिसेंटिंग ओपिनियन। ही गेव द फॉलोविंग पॉइंट्स)-
- जिस तरह से राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति को चुनौती (चैलेंज) दी जा सकती थी, वह एकमात्र तरीका दुर्भावनापूर्ण (मलाफाइड) और भ्रष्ट (करप्ट) इरादों के आधार पर था। तथ्य यह है कि अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने से ठीक दो दिन पहले जारी किया गया था, यह दर्शाता है कि इसे वैध रूप से पारित किया गया था, लेकिन जल्दबाजी में।
- अध्यादेश के ठीक पहले कुछ दिनों के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सरकार की मंशा के बारे में देश में काफी अटकलें (स्पेकूलेशन) थीं।
- कारण स्पष्ट है कि जिस प्रकार नीति (पॉलिसी) के मामलों में संसद अपने प्रांत की स्वामी (मास्टर) होती है, उसी प्रकार राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर ऐसे नीतिगत मामलों पर अपनी संतुष्टि (सेटिस्फेक्शन) का सर्वोच्च और एकमात्र न्यायाधीश होता है।
- उन्होंने कई अन्य कारणों से याचिकाओं को खारिज कर दिया और इस प्रकार, याचिकाओं को विफल (फेल) घोषित कर दिया।
- एक शेयरधारक अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकता है, जो अंत में एक कंपनी से जुड़ा था, जो एक गैर-नागरिक (नॉन सिटिज़न) होने के कारण मौलिक अधिकारों का दावा करने का अधिकार नहीं रखता था।
- एके गोपालन मामले में प्रतिपादित ‘पारस्परिक विशिष्टता सिद्धांत’ (म्युचल एक्सक्लूजिवीटी थिअरी) को उनके द्वारा सही ठहराया गया था।
हालाँकि, वास्तव में दो बातें थीं जिन पर वह बहुमत से सहमत (सहमत) थे और वे थीं-
- कि आक्षेपित अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं है, जो किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता को रोकता है।
- कि संसद बैंकिंग के अधिग्रहण से संबंधित आक्षेपित अधिनियम को पारित करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम (कौंपीटेंट) थी।
जटिल अन्वेषण (क्रिटिकल एनालिसिस)
बहुत से लोग इस मामले को राष्ट्र के समाजवादी आदर्शों के खिलाफ जाने से भ्रमित (भ्रमित) करते हैं। हालाँकि, यह समझना चाहिए कि वास्तव में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीयकरण की सरकार की शक्ति को बरकरार (अपहेल्ड) रखते हुए संविधान के समाजवादी आदर्शों को बरकरार रखा था। हालांकि, यह भी याद रखना चाहिए कि न्यायालय ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के दायरे में यह फैसला सुनाया कि उल्लंघन की प्रक्रिया में, शेयरधारक के मौलिक अधिकारों को लागू करने के दावे को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं था, अगर उनके अधिकारों कके साथ, उनकी कंपनी के अधिकारों का भी उल्लंघन किया जा रहा था।
यह समझा गया कि यदि शेयरधारक के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जाना था, तो इस प्रक्रिया में, इसका मतलब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय अनिवार्य रूप से उस कंपनी के अधिकारों को भी लागू कर रहा था जिसमें वह एक शेयरधारक था, जिसका अर्थ है कि मौलिक अधिकार एक गैर-नागरिक के लिए लागू किया जा रहा था। लेकिन, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भले ही शेयरधारक के मौलिक अधिकारों को लागू करने का मतलब कंपनी के अधिकारों को लागू करना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने से नहीं रोकेगा, भले ही इस प्रक्रिया में कुछ अवांछित प्रवर्तन (अनवांटेड इन्फोर्समेंट) हो रहा था।
इसके अलावा, यह मामला एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने पारस्परिक विशिष्टता सिद्धांत को खारिज कर दिया था जिसे ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में प्रतिपादित (प्रोपौंड) किया गया था। इसने उल्लेख किया कि सभी अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए (इंटरलिंक) थे और न्यायशास्त्र (जुरिसप्रूडेंस) के प्रयोजनों के लिए अलग से व्यवहार नहीं किया जा सकता था।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक और ऐतिहासिक बिंदु (लैंडमार्क पॉइंट) संसद को कानून बनाने की लंबी प्रक्रियाओं से मुक्त करने के संबंध में था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि किसी भी विषय के राष्ट्रीयकरण पर कोई कानून बनाने के लिए, इसका मतलब यह नहीं था कि संसद को पहले उस विषय पर एक अलग कानून बनाना होगा और फिर उसके राष्ट्रीयकरण के संबंध में कानून बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा, जैसा कि इसने संपत्ति शब्द की व्याख्या का विस्तार किया जो राज्य सूची की प्रविष्टि 42 के तहत थी।
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला वास्तव में संसद का मार्गदर्शन (गाइडिंग) करने के साथ-साथ आने वाले वर्षों के लिए देश के संवैधानिक न्यायशास्त्र (कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसप्रूडेंस) के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, फैसले के बाद शायद इस तथ्य से ध्यान दिया गया कि संसद ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, 25 वां संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम (25थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट) बनाया, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया-
- अनुच्छेद 31(2) में ‘मुआवजा’ शब्द को ‘राशि’ शब्द से बदल दिया गया था। इसका मतलब यह था कि सरकार अब उस व्यक्ति को ‘पर्याप्त’ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी जिसकी संपत्ति पहले की तरह अर्जित (एक्विजिशन) की जा रही थी।
- अनुच्छेद 19(1)(g) स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 31(2) से अलग था।
- अनुच्छेद 31सी, सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया कि-
- अनुच्छेद 39 (बी) और 39 (सी) के तहत निर्धारित उद्देश्यों (ऑब्जेक्टिव) को पूरा करने के लिए उसके तहत बनाए गए किसी भी कानून पर अनुच्छेद 14, 19 और 31 लागू नहीं होंगे।
- अनुच्छेद 39 (बी) और 39 (सी) को प्रभावी करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय के हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) से प्रतिरक्षित (इम्यून) किया जाएगा।
इसलिए, यह सब आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ का मामला, लोकप्रिय रूप से 1970 के बैंक राष्ट्रीयकरण मामले के रूप में जाना जाता है।
संदर्भ (रेफरेंसेस)
- Rustom Cavasjee Cooper Vs. Union of India, 1970 AIR 564, https://indiankanoon.org/doc/513801/
- Hemant Varshney, R.C. Cooper Vs. Union of India- Bank Nationalisation Case- Case Summary, Law Times Journal, (Sep. 27, 2018), http://lawtimesjournal.in/r-c-cooper-v-union-of-india-bank-nationalization-case-case-summary/
- Anonymous, R.C. Cooper Vs. Union of India, The Bank Nationalisation Case, A Turning Point in the Interpretation of Fundamental Rights, http://www.jurisedge.com/wp-content/uploads/RC%20Cooper%20Presentation.pdf