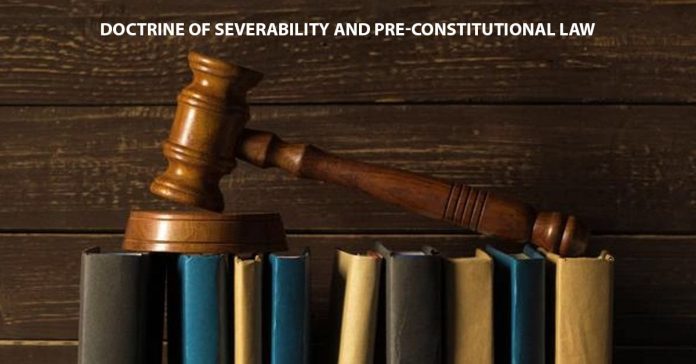यह लेख नोएडा के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की बीबीए एलएलबी की छात्रा Heba Ali द्वारा लिखा गया है। यह लेख विच्छेदनीयता (सेवरेबिलिटी) के सिद्धांत और इसकी विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
सिद्धांत का आधार
विच्छेदनीयता के इस सिद्धांत को पृथक्करणीयता (सेपरेबिलिटी) के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। शब्द “असंगति या उल्लंघन की हद तक” यह स्पष्ट करता है कि जब किसी क़ानून के कुछ प्रावधान मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता के कारण असंवैधानिक हो जाते हैं, तो प्रश्नगत कानून के केवल प्रतिकूल प्रावधान को ही अदालतों द्वारा शून्य माना जाएगा, न कि पूरे क़ानून को।
विच्छेदनीयता के सिद्धांत का अर्थ है कि जब किसी क़ानून का कोई विशेष प्रावधान किसी संवैधानिक सीमा का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध होता है, लेकिन वह प्रावधान शेष क़ानून से अलग करने योग्य है, तो केवल उस आपत्तिजनक प्रावधान को न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा, न कि संपूर्ण क़ानून को।
विच्छेदनीयता का सिद्धांत कहता है कि यदि ‘और’ या ‘या’ शब्द का उपयोग करके अच्छे और बुरे प्रावधानों को एक साथ जोड़ा जाता है और अच्छे प्रावधान के प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) को बुरे के प्रवर्तन पर निर्भर नहीं किया जाता है, तो अच्छा प्रावधान लागू किया जा सकता है भले ही बुरा अस्तित्व में न हो, दो प्रावधान अलग-अलग हैं और अच्छे को मान्य और प्रभावी माना जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई प्रावधान है जो कानूनी उद्देश्य के साथ-साथ अवैध उद्देश्य के लिए उपयोग करने में सक्षम है, तो यह अमान्य है और कानूनी उद्देश्य के लिए भी इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
इस सिद्धांत में, संपूर्ण अधिनियम को संविधान के भाग तीन के साथ असंगत होने के कारण अमान्य नहीं माना जाता है, जो भारत के नागरिकों को दिया जाता है। यह केवल वे हिस्से होते हैं जो असंगत हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन केवल वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उससे अलग किया जा सकता है जो उन्हें अलग नहीं करता है। यदि यह है कि वैध भाग को अमान्य भाग के साथ जोड़ दिया जाए तो उन्हें अलग करना असंभव है। तब ऐसे मामलों में न्यायालय उसे छोड़ देगा और पूरे अधिनियम को ही शून्य घोषित कर देगा। इसे करने की इस प्रक्रिया को विच्छेदनीयता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के.गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में इस सिद्धांत का प्रयोग किया है, यह अदालत द्वारा आयोजित किया गया था कि निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 से हटा दिया जाना चाहिए, तब यह वैध होगा और इसे हटाने से अधिनियम प्रभावित नहीं होगा और यह मान्य और प्रभावी रहेगा। इस सिद्धांत को आगे डीएस नकरा बनाम भारत संघ में भी लागू किया गया था जहां यह हुआ था कि अधिनियम वैध रहा और जो हिस्सा सुसंगत नहीं था उसे अमान्य घोषित कर दिया गया और ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आसानी से वैध भाग से अलग हो गया था। साथ ही, बॉम्बे राज्य बनाम एफ एन बलसारा में यह माना गया कि बंबई निषेध अधिनियम, 1949 के प्रावधान को शून्य घोषित किया गया था, लेकिन इसने बाकी हिस्से को प्रभावित नहीं किया और इसलिए पूरे क़ानून को शून्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
विच्छेदनीयता के सिद्धांत का उपयोग मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में भी किया गया था, जहां 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 4 और 55 को संसद की संशोधन शक्ति से परे होने के कारण रद्द कर दिया गया था और फिर इसने शेष अधिनियम को वैध घोषित कर दिया था। फिर किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु के एक अन्य मामले में, जो दल-बदल मामले के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ है, 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा पहली बार डाली गई दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक घोषित किया गया था क्योंकि इसने अनुच्छेद 368(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। लेकिन, पूरे हिस्से को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया। इसलिए, पैराग्राफ 7 को छोड़कर बाकी दसवीं अनुसूची को संविधान द्वारा बरकरार रखा गया था।
आर.एम.डी.सी बनाम भारत संघ के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विच्छेदनीयता के सिद्धांत पर विचार किया गया था और इस मामले में विच्छेदनीयता के नियम निर्धारित किए गए थे, जो निम्नलिखित है-
- इसके पीछे विधायिका की मंशा यह निर्धारित करना है कि क़ानून के अवैध हिस्से को वैध हिस्से से अलग किया जा सकता है या नहीं।
- और यदि ऐसा होता है कि वैध और अमान्य दोनों भागों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, तो क़ानून के हिस्से की अमान्यता के परिणामस्वरूप पूरे अधिनियम की अमान्यता हो जाएगी।
- भले ही ऐसा होता है कि अमान्य भाग मान्य भाग से अलग है।
यह अदालतों की शक्ति और कर्तव्य है कि वे कानून जो भारत के संविधान के साथ असंगत है को असंवैधानिक घोषित करें। न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) की इस शक्ति का आधार, जैसा कि नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह सिद्धांत समझाया गया था कि, हमारा संविधान जो इस भूमि का मौलिक कानून है, और साथ ही लोगों की इच्छा है, लेकिन क़ानून केवल लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का निर्माण है, इसलिए जब किसी क़ानून में घोषित विधायिका की इच्छा, संविधान में घोषित लोगों के विरोध में खड़ी होती है, तो लोगों की इच्छा प्रबल होनी चाहिए।
साथ ही, संविधान का उल्लंघन करने वाले कार्यपालिका (एक्जीक्यूटिव) और न्यायपालिका के कार्यों को रद्द करने की शक्ति स्वयं संविधान द्वारा न्यायपालिका में दी गई है। लेकिन, यही विधायिका का हिस्सा नहीं है जिसे संविधान द्वारा बनाया गया है या जिसे कानून बनाने वाली संस्था कहा जाता है। यह कहना सही नहीं है कि विधायकों का मत प्रबल होना चाहिए क्योंकि वे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। एक प्रावधान की संवैधानिकता का निर्धारण करने में अदालत पहले सवाल करेगी कि क्या कानून संवैधानिक है या नहीं क्योंकि इस बात की संभावना हो सकती है कि यह संविधान में निहित बहुत सारे अनुच्छेदो का उल्लंघन कर रहा हो।
विच्छेदनीयता के सिद्धांत का अभ्यास
विच्छेदनीयता के सिद्धांत का अभ्यास बहुत लंबे समय से चलन में है और यह कोई नई बात नहीं है। इसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया जैसे कई देशों में अपनाया गया है और इसी तरह हमारे देश भारत में भी अपनाया गया है। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में विच्छेदनीयता का सिद्धांत वापस चला जाता है जब इसकी उत्पत्ति नॉर्डेनफेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्डेनफेल्ट गन्स एंड एम्युनिशन कंपनी लिमिटेड के मामले में हुई थी। इस विशेष मामले में मामला अमेरिकी संविधान के पंद्रहवें संशोधन के आसपास केंद्रित था जिसमें रंग या जाति आदि के आधार पर अमेरिकी पुरुष नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं करने की बात कही गई थी।
फिर चम्पलिन रिफाइनिंग कंपनी बनाम कॉर्पोरेशन कमीशन ऑफ ओक्लाहोमा के बहुत लोकप्रिय मामले में जहां एक तेल शोधन कंपनी ने ओक्लाहोमा क़ानून के कई प्रावधानों को चुनौती दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि विभिन्न प्रावधानों ने वाणिज्य (कॉमर्स) खंड और यहां तक कि चौदहवें संशोधन का उल्लंघन किया था जो उचित प्रक्रिया और समान सुरक्षा खंडों के बारे में बात करता है। और यह निर्धारित किया कि क्या इनमें से किसी को या इनमें से किसी एक को खत्म किया जा सकता है और मुद्दे पर तेल और गैस क़ानून के अवशेष से अलग किया जा सकता है। वर्ष 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्निहित तर्क के रूप में तीन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। फिर अयोटे बनाम प्लेनड पैरेंटहुड ऑफ नॉर्दन न्यू इंजीनियरिंग के मामले में भी अदालत ने विच्छेदनीयता के तीन सिद्धांतों को निर्धारित किया था।
एक अन्य मामले में जो कार्डेग्ना बनाम बकेई चेक कैशिंग का है जो कि वर्ष 2006 में सामने आया था, जहां प्रतिवादी जो कि बकेई था, ने एक सहायक कंपनी से ऋण राशि ली थी, जो एक व्यवसाय था। बाद में उसने फिर से एक और ऋण राशि ली जो पहले ली गई ऋण राशि से अधिक थी और बाद में वह उसका भुगतान करने में असमर्थ था। फिर उन्होंने एक वकील की मदद से क्लास एक्शन वाद दायर किया। वाद के संबंध में मुद्दा यह था कि वादी द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें अन्य की तुलना में अधिक थीं जो कि कंपनी द्वारा चार्ज की गई थी और जो निर्धारित सामान्य दरों से कम से कम 45 प्रतिशत अधिक थी। लेकिन, फ्लोरिडा की अदालत ने कहा कि यह अनुबंध का केवल एक हिस्सा नहीं है जिसे चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इसे पूरे अनुबंध की आवश्यकता है। और इसलिए इसका मतलब यह है कि विच्छेदनीयता का सिद्धांत जो पहले सोचा जाता था कि लागू किया जा सकता है अब लागू नहीं किया जा सकता है। आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और घोषित किया कि संपूर्ण अनुबंध इस आधार पर शून्य था क्योंकि ऐसे शून्य अनुबंध, अपने प्रारंभिक चरण से ही बिल्कुल शून्य और बेकार होते हैं।
विच्छेदनीयता का सिद्धांत अब केवल पश्चिमी दुनिया का हिस्सा रहा है, बल्कि दुनिया के पूर्वी देशों में भी फैल गया है। जैसे भारत से मलेशिया और मलेशिया में यह सिद्धांत बहुत लोकप्रिय मामले में विकसित हुआ था जो कि मलेशियाई बार और अन्य बनाम मलेशिया सरकार का है। जब हम विच्छेदनीयता के सिद्धांत के संबंध में भारत के बारे में बात करते हैं तो हमें यह अध्ययन करने और समझने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 कैसे अस्तित्व में आया था। यह सिद्धांत तब काम करता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून का कोई भी भाग संविधान का उल्लंघन करता है। जब हम भारतीय संविधान के संदर्भ में बात करते हैं तो यह मौलिक अधिकार होंगे जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं। इसलिए, यह सिद्धांत विशेष रूप से तब काम करेगा जब यह भारतीय संविधान के भाग III के अधीन होगा।
क्या कोई कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे सकता है
कोई भी व्यक्ति कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे सकता है, लेकिन तभी जब उसके अधिकार कानून से सीधे प्रभावित होते हैं। तभी कोई भी व्यक्ति कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठा सकते हैं। यह इस प्रकार है-
जब कोई व्यक्ति उस वर्ग से बाहर होता है जहां वह क़ानून से आहत हो सकता है तो उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर जहां कोई क़ानून बोना वेसेंटिया (यानी वह स्थिति जिसमें संपत्ति बिना किसी स्पष्ट स्वामी के रह जाती है) को प्रभावित करता है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऐसी क़ानून की वैधता को चुनौती देने के लिए सक्षम हो। फिर से, जहां क़ानून एक अनुबंध के रूप में संचालित होता है, अनुबंध के लिए कोई भी पक्ष क़ानून की वैधता को चुनौती देने का हकदार है।
न्यायालयों द्वारा ली गई उपधारणा (प्रिजंप्शन)
यह हमेशा उस व्यक्ति पर होती है जो यह दिखाने की कोशिश करता है कि यह संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो यह वह है जिस पर अदालतों को यह दिखाने का भार है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय इसके संवैधानिक सिद्धांत हैं और इसके निर्णय दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं, जैसा कि चिरंजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में कहा गया था। यदि ऐसा होता है कि चुनौती संविधान के प्रावधानों पर नहीं है, तो अदालतों को इस पर विचार करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह अधिकारातीत (इंट्रा वायर्स) है और उसी की व्याख्या करने का प्रयास करें। इसलिए, यह स्पष्ट है कि बोझ पूरी तरह से उस व्यक्ति पर है जो निर्णय पर सवाल उठाता है और इसे कानून की अदालत में चुनौती देता है।
अगर कुछ होता है और अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है, तो व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि उसके परिणामस्वरूप उसे कुछ चोट लगी है या कानून के प्रभाव में आने के परिणामस्वरूप उसे कुछ प्रत्यक्ष चोट लगने का तत्काल खतरा है। और अगर यह किसी भी रूप में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो पीड़ित व्यक्ति के पास राज्य द्वारा कुछ या किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की प्रतीक्षा या देरी किए बिना अदालतों में जाने की सभी शक्तियाँ हैं। और यदि ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है तो वह कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकता है कि यह मौलिक अधिकार के साथ असंगत है। यहां तक कि एक निगम के पास अपने शेयरधारकों से अलग एक कानूनी इकाई होती है। इसलिए, निगमों के मामले में, चाहे निगम स्वयं या शेयरधारक क़ानून की वैधता पर आरोप लगाने के हकदार होंगे और यह इस सवाल पर निर्भर करेगा कि क्या निगम या शेयरधारकों के अधिकार क़ानून से प्रभावित हुए हैं।
जब ऐसा होता है कि कंपनी के मौलिक अधिकारों को क़ानून द्वारा लागू किया जाता है तो यह संबंधित शेयरधारकों के हितों को भी प्रभावित करता है, ऐसे मामलों में शेयरधारक क़ानून की संवैधानिकता को भी चुनौती देते हैं। ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि सह-याचिकाकर्ता के रूप में कंपनी का ज्वाइंडर शेयरधारकों को राहत नहीं देगा, भले ही कंपनी ‘नागरिक’ न हो और इसलिए राहत की हकदार नहीं होगी। साथ ही, सरकार द्वारा कंपनी के प्रबंधन को ले लिए जाने के कारण वित्तीय राहत की संभावना एक शेयरधारक को लोकस स्टैंडी देने के लिए पर्याप्त है।
प्रभाव जब एक कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाता है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है जो भारत के क्षेत्र के भीतर हैं। उदाहरण के लिए, एक बार यदि कोई कानून भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो उस तारीख से यह भारत की सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होगा। इसका प्रभाव यह है कि निर्णय उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णय के रूप में कार्य करता है जो भारत में किसी भी न्यायालय में राहत प्राप्त कर सकते हैं या करने जा रहे हैं। इसलिए, आगे की कार्यवाही में फिर से अपनी असंवैधानिकता को स्थापित करने के लिए प्रभावित होने वाले पक्ष पर कोई दायित्व नहीं है और फिर अदालत उस कानून को खारिज करने के लिए बाध्य है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया गया है।
याही बात तब लागू होती है जब कानून को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया गया हो। यदि किसी मामले में कानून को लागू करने की मांग की जाती है तो ऐसे मामलों में उस हिस्से का न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नहीं लिया जाता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है कि न्यायालय क़ानून को इस तरह से पढ़ेगा कि धारा का वह भाग जिसे अमान्य घोषित किया गया है, पहले कभी मौजूद नहीं था। यदि ऐसा होता है कि उस व्यक्ति पर उस धारा के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाता है जिसे अमान्य घोषित किया गया है, तो अभियुक्त पर यह साबित करने का कोई दायित्व नहीं है कि उसका मामला उस धारा के तहत आता है जिसे अमान्य ठहराया गया है। दूसरी ओर ऐसा होता है कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि अभियुक्त ने धारा के उस भाग का उल्लंघन किया है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् प्रवर्तनीय और वैध है।
कोई अंतर नहीं किया जाता है जहां विधायी क्षमता की कमी के कारण कानून को अमान्य घोषित किया जाता है और ऐसे मामले में जहां इसे मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित किया जाता है। यहां तक कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 245 (1) बहुत ही विशेष रूप से बताता है कि विधायी शक्ति चाहे वह संघ की हो या राज्य विधानमंडल की हो, हमेशा ही संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहेगी। इसका परिणाम यह होता है कि जब कोई विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, जैसे कि कोई मौलिक अधिकार तो स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे कि उनके पास कानून की विषय-वस्तु पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं थी। फिर, तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की अमान्यता की घोषणा दोनों में से किसी भी मामले में विधायी शक्ति के माध्यम से होती है, जैसा कि स्वयं न्यायालय द्वारा कई मामलों में आयोजित किया गया था।
संवैधानिक संशोधन के कारण असंवैधानिक क़ानून पर प्रभाव
पहले के दिनों में इस विषय पर बहुत भ्रम था जब एक संवैधानिक संशोधन होता है और इस वजह से असंवैधानिक क़ानून पर कुछ प्रभाव पड़ता है। पूर्व-संविधान कानून के मामले में ‘आच्छादन (एक्लिप्स) के सिद्धांत’ को लागू किया जा सकता है जो कि लागू होने पर मान्य था। लेकिन, अगर संविधान के साथ कुछ असंगति थी जो बाद में अस्तित्व में आई, और जब छाया हटा दी जाती है, तो संविधान-पूर्व कानून सभी प्रकार की दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है।
लेकिन बात यह है कि सिद्धांत को संविधान के बाद के कानून के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है जो कि शुरू से ही शून्य है। अनुच्छेद 13(2) को ध्यान में रखते हुए, मौलिक अधिकार संविधान के प्रारंभ के बाद कानून बनाने वाली विधायिका की विधायी शक्ति पर अभिव्यक्त सीमाएँ बनाते हैं और संविधान के बाद के कानून के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जो कि अधिकारातीत (अल्ट्रा-वायर्स) है जो विधायिका की विधायी क्षमता से परे है और एक कानून जो एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। संविधान के बाद के कानून के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है जो कि अधिकारातीत है। यह है कि एक बाद वाला संवैधानिक कानून जो एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, शुरू से ही शून्य है और संविधान का कोई भी बाद का संशोधन इस तरह के जन्मजात कानून को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, जब तक कि ऐसा संशोधन पूर्वव्यापी (रेस्ट्रोस्पेक्टिव) न हो।
विधायिका की शक्ति जब एक क़ानून को असंवैधानिक घोषित किया जाता है
जब किसी क़ानून को अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो विधानमंडल सीधे उस निर्णय को रद्द नहीं कर सकता है जो लिया जाता है और क़ानून को फैसले की तारीख पर वैध घोषित करता है। हालांकि, यह इसलिए है कि एक नए कानून के लिए विधानमंडल की क्षमता जो आगे असंवैधानिकता से मुक्त है और फिर प्रदान करता है कि आपत्तिजनक कानून के तहत किया गया कुछ भी नए कानून के तहत माना जाएगा और इसके प्रावधानों के अधीन होगा।
असंवैधानिक क़ानून पर आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव
आपातकाल की उद्घोषणा जो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, इसके संचालन में संभावित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 358 जो विधायिका को उस सीमा से मुक्त करता है जो अनुच्छेद 19 में आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान इसकी निरंतरता के दौरान रखी गई है। लेकिन यह उस कानून को मान्य करने के लिए काम नहीं करता है जो उद्घोषणा से पहले अधिनियमित किया गया था जो कि अनुच्छेद 13(2) के उल्लंघन के कारण अमान्य था। तब ऐसे कानून शुरू से ही शून्य हो जाएंगे और आपातकाल की उद्घोषणा द्वारा पुनर्जीवित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए, अब यदि कोई कार्यकारी कार्रवाई जो इस तरह के शून्य कानून द्वारा हाथों में किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है, वह भी अमान्य होगी, भले ही इस तरह की कार्रवाई उद्घोषणा के शुरू होने या पूर्व-संविधान कार्यकारी कार्रवाई के जारी रहने के बाद होती है।
क्या एक अधिकार छोड़ा जा सकता है
महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्षों से रहा है वह यह था कि क्या एक मौलिक अधिकार को छोड़ा जा सकता है जिसका उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिया है। उदाहरण के लिए बेहराम बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में जहां माननीय न्यायाधीश वेंकटराम ने यह विचार व्यक्त किया था कि ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के लिए और उनके हित में हैं और आम जनता के हित से पूरी तरह भिन्न है, तदनुसार अनुच्छेद 19(1) द्वारा गारंटी अधिकार भी छोड़ा जा सकता है जो कि इसी श्रेणी में आता है।
लेकिन बाकी सभी के पास वही दृष्टिकोण नहीं था जो बहुमत है जिसमें मुख्य न्यायाधीश महाजन मुखर्जी, बोस और हसन शामिल थे। और उन्होंने उस प्रश्न का निर्णय किए बिना भी दृष्टिकोण व्यक्त किया जो मुख्य रूप से व्यक्तियों की भलाई के लिए था। इसे हमारे संविधान में सार्वजनिक नीति के आधार पर और प्रस्तावना में ही घोषित उद्देश्य के अनुसरण में भी रखा गया है। तो, अंत में निष्कर्ष यह है कि मौलिक अधिकारों में से कोई भी माफ नहीं किया जा सकता है।
फिर बशेशर बनाम कमिश्नर ऑफ आईटी के मामले में न्यायमूर्ति भगवती और सुब्बा राव ने यह माना है कि एक मौलिक अधिकार राज्य को संबोधित एक निषेध की प्रकृति में है, हमारे संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को एक व्यक्ति द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है और यह घोषणा बहुमत द्वारा हैबेहराम के मामले में देखी गई।
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे कॉर्पोरेशन के बहुत प्रसिद्ध मामले में संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा है कि देश के सर्वोच्च कानून संविधान के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। साथ ही, कोई व्यक्ति स्वयं संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता है जो कि भाग III में वर्णित है। कई मामलों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अदालतों ने छूट के सवाल पर भी विचार किए बिना, अदालत ने माना है कि एक व्यक्ति जिसने एक अधिनियम द्वारा कार्यालय में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, उसे इस आधार पर चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता है कि यह उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जिसकी गारंटी अनुच्छेद 16 के अधीन है।
स्वीकृति का प्रभाव
पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां यह माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने कानून के तहत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त किया है तो वह किसी भी मामले में इसकी संवैधानिकता या इसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकता है। जैसे नैन सुख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया है कि एक व्यक्ति जिसे एक चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, जो सांप्रदायिक आधार पर गठित अलग निर्वाचक मंडल के आधार पर किया जा रहा है, तो वह चुनाव के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपचार की तलाश नहीं कर सकता है।