यह लेख Prashant Prasad द्वारा लिखा गया है। यह अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, मुद्दों और तर्कों, इसमें शामिल विभिन्न कानूनी पहलुओं और के.सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य (1953) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है। लेख उड़ीसा संपदा (एस्टेट) उन्मूलन (अबॉलिशन) अधिनियम, 1952 और अन्य प्रासंगिक कानूनी अवधारणाओं से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर गहराई से चर्चा करता है, जिससे पूरे मामले की व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव) समझ मिलती है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
1952 में, उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम (इसके बाद “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) पेश किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और भूमि को राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में लाना था। सरकार बिचौलियों (इंटरमीडिएरीज़) को हटाने और भूमि किसानों और किरायेदारों (टेनेंट्स) को राज्य के सीधे संपर्क में लाने के लिए ऐसा अधिनियम लेकर आई। ऐसे अधिनियम के प्रावधानों से व्यथित भूमिधारकों (लैंडहोल्डर्स) ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।
वर्तमान मामला भूमि सुधार पर सरकार के कानून और भूमिधारकों के अपनी भूमि पर पारंपरिक अधिकारों के बीच टकराव को उजागर करता है। इस अधिनियम ने समाज में सामाजिक परिवर्तन लाए, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही पारंपरिक प्रथा के विपरीत है। इस विशेष मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अधिनियम को बरकरार रखा और भूमिधारकों द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय से व्यथित होकर, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई और अंत में, के.सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य (1953) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया। वर्तमान मामला इस तथ्य को दर्शाता है कि न्यायपालिका सामाजिक न्याय के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ किसी व्यक्ति के अधिकारों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
यह मामला भूमि स्वामित्व में सुधार और अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण के प्रयासों को दर्शाता है ताकि भूमि दक्षता को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। वर्तमान मामले में न्यायपालिका इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने का प्रयास करती है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, न्यायसंगत और उचित मुआवजा, और अन्य प्रासंगिक अवधारणाएँ जो संपत्ति से संबंधित अधिकारों को समझने के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान मामले के आधार पर, भूमि सुधार पर कानून बनाने की राज्य की क्षमता के संबंध में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की गई है।

मामले का विवरण
- मामले का नाम: के.सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य
- अपीलकर्ता: के.सी. गजपति नारायण देव और अन्य
- प्रतिवादी: उड़ीसा राज्य
- न्यायालय का नाम: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- न्यायाधीशों की पीठ: माननीय एम. पतंजलि शास्त्री (मुख्य न्यायाधीश); माननीय बी.के. मुखर्जी; माननीय सुधी रंजन दास; माननीय गुलाम हसन और माननीय एच नटवरलाल भगवती
- मामले का प्रकार: सिविल अपील
- निर्णय की तिथि: 29/05/1953
- समतुल्य उद्धरण (साइटेशन): 1954 एससीआर 1, 1953 एआईआर 375
मामले के तथ्य
वर्तमान मामले में, उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 17 जनवरी 1950 को उड़ीसा राज्य द्वारा पेश किया गया था और 28 सितंबर 1951 को उड़ीसा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था और अंततः, 23 जनवरी 1952 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। सहमति के बाद, अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(4) और अनुच्छेद 31A (विशेष रूप से अनुच्छेद 31A के खंड (1) के उप-खंडों के तहत) के तहत सुरक्षा प्राप्त होती है। हालाँकि, इसे नौवीं अनुसूची के तहत उल्लिखित क़ानूनों की सूची में शामिल नहीं किया गया था (संविधान की नौवीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची शामिल है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है)। वर्तमान अधिनियम बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश विधानसभाओं (यानी बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950, मध्य प्रदेश मालिकाना अधिकार उन्मूलन अधिनियम, 1950 आदि) में पारित क़ानून के समान स्वरूप का अनुसरण करता है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सभी बिचौलियों को समाप्त करके सभी जमींदारी और मालिकाना सम्पदाओं को समाप्त करना था ताकि भूमि के वास्तविक कब्जेदारों को राज्य सरकार के सीधे संपर्क में लाया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों से व्यथित सम्पदाओं के मालिकों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष छह अपीलें दायर कीं।
अपीलकर्ता ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष अधिनियम की असंवैधानिकता के बारे में कई आधार प्रस्तुत किए। अपीलकर्ता का मानना था कि वर्तमान अधिनियम एक छदम कानून (कलरेबल लेजिस्लेशन) है, क्योंकि इसमें सरकार द्वारा विधायी शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया गया है। न्यायालय का मत था कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश विधानसभाओं के समान कानून की वैधता के प्रश्न पर न्यायालय ने विचार किया था, और बिहार अधिनियम के कुछ मामूली प्रावधानों को छोड़कर सभी को न्यायालय ने संवैधानिक माना था। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क को उड़ीसा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (माननीय एम. पतंजलि शास्त्री) द्वारा तीन शीर्षकों के तहत निर्णय में वर्गीकृत किया गया था। पहले शीर्षक के तहत, अधिनियम की संवैधानिक वैधता के बारे में विवाद उठाए गए थे। दूसरे शीर्षक के अंतर्गत, अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संपदा में शामिल संपत्ति की कुछ वस्तुओं से संबंधित है, जैसे निजी भूमि, भवन, बंजर भूमि, आदि। अंत में, अधिनियम को चुनौती देने का आधार अधिनियम के कुछ प्रावधानों से संबंधित है, जो अधिनियम की धारा 37 के तहत मध्यस्थों को देय मुआवजे के निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में है, जो सकल परिसंपत्तियों की गणना या शुद्ध आय पर पहुंचने के लिए की जाने वाली कटौती के संदर्भ में है।
एक विस्तृत निर्णय में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा की तथा कुछ को छोड़कर शेष सभी दलीलों को खारिज कर दिया, जिन पर आगे चर्चा की जा सकती है। पीठ के एक अन्य विद्वान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नरसिम्हन, अधिकांश बिंदुओं पर मुख्य न्यायाधीश से सहमत थे। हालांकि, उन्होंने उड़ीसा कृषि आयकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1950 के बारे में अपनी अलग राय व्यक्त की। उनके अनुसार, यह अधिनियम एक कर उपाय प्रतीत होता है, लेकिन यह बिचौलियों की आय को कम करने का प्रयास कर सकता है, और इसलिए आगे की शुद्ध आय कम हो सकती है। वर्तमान मामले के विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद, अंततः उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अधिनियम को संवैधानिक माना। निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 133 के तहत अपील दायर की।

उठाए गए मुद्दे
- क्या उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 संवैधानिक रूप से वैध है?
- क्या उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952, छदम कानून का एक हिस्सा है?
- क्या मालिकों को मुआवज़ा देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया वैध है?
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता
अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा कई तर्क उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- वर्तमान अधिनियम के तहत देय मुआवजे का निर्धारण करने के लिए दो कानूनों अर्थात् उड़ीसा कृषि आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1947 और मद्रास संपदा भूमि (संशोधन) अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की वैधता के बारे में प्रश्न उठाए गए थे, क्योंकि वे किसी संपदा की शुद्ध आय की गणना को प्रभावित करते हैं। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसा कानून बिल्कुल भी वास्तविक कानून नहीं है, बल्कि यह महज छदम कानून का एक हिस्सा है, क्योंकि इस कानून का वास्तविक उद्देश्य मध्यस्थों की शुद्ध आय को कम करना है।
- अधिनियम के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई क्योंकि वे स्वामी की निजी भूमि और भवनों पर लागू होते हैं, जो अधिनियम की धारा 5 के अनुसार संपदा का हिस्सा हैं।
- अधिनियम की धारा 37 के अनुसार जिस तरीके से मुआवजा दिया जाता है, उसे अवैध और असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई है।
- उपर्युक्त तर्कों के साथ-साथ, वकील ने बिहार राज्य बनाम महाराजा कामेश्वर सिंह और अन्य (1952) के मामले पर भरोसा किया, जिसमें बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(b) और धारा 23(f) के दो प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक माना गया था कि प्रावधान संविधान के साथ धोखाधड़ी करता है। वकील ने यूनियन कोलियरी कंपनी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया लिमिटेड बनाम बायर्डन (1899) के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें “छदमता का सिद्धांत” विचार के लिए आया था।
प्रतिवादी
अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के जवाब में, विद्वान महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) ने तर्क दिया कि –
- अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
- आगे यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क अधिनियम की वैधता पर हमला करने का आधार नहीं हैं।
- देय किराये के आधार पर सकल परिसंपत्तियों की गणना से संबंधित अधिनियम के प्रावधान अवैध नहीं हैं।
- यदि अपीलकर्ताओं की दलीलें सही हैं, तो वे अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय किराये के आधार पर सकल परिसंपत्तियों की गणना के संबंध में आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- यदि अधिनियम के तहत किराये की गणना के लिए निर्धारित नियम अमान्य पाया जाता है, तो निर्धारित किराया खारिज कर दिया जाएगा, और अपीलकर्ता को पिछले वर्ष के किराये को तय किराये के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी।
इस मामले में शामिल कानूनी प्रावधान और अवधारणाएँ
छदमता का सिद्धांत
इस सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्धांत इस मामले के मुद्दों में से एक में शामिल है। छदमता का सिद्धांत, एक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा विधायी शक्ति के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। इस सिद्धांत का प्राथमिक उपयोग संबंधित कानून पर विधायिका की योग्यता की जांच करना है। इस सिद्धांत को उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जब विधायिका किसी विशेष मामले पर कुछ कानून बनाने में सक्षम नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस विषय पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाती है। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां कानून मुख्य रूप से विधायिका की संवैधानिक शक्ति के भीतर प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में, यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र से परे उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास हो सकता है। उस परिदृश्य के तहत, इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।
छदमता का सिद्धांत लैटिन कहावत से लिया गया है – “क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबेटुर एक्स डायरेक्टो, प्रोहिबेटुर एट पेर ओब्लिकम” जो इस उद्देश्य पर आधारित है कि विधायिका की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक सीमा के भीतर किया जाना चाहिए और यदि उस सीमा को पार करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो ऐसे विधान को छदम विधान का एक हिस्सा माना जाएगा। इसलिए, यह सिद्धांत न्यायपालिका को यह सत्यापित करने का अधिकार देता है कि विधान क्षेत्राधिकार की आवश्यकता के अनुपालन में है या नहीं। इसलिए, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि विधायिका कुछ कानूनों को सीधे लागू नहीं कर सकती है, तो वे ऐसे कानूनों को लागू करने के लिए कोई अप्रत्यक्ष तरीका भी नहीं अपना सकते हैं।
छदमता के सिद्धांत के बारे में अधिक जानने के लिए यहां दबाये।

उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952
मामले और इससे जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता के लिए न्यायालय द्वारा उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। अधिनियम के कुछ चर्चित प्रावधान इस प्रकार हैं:
उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 3
यह धारा किसी संपत्ति की अधिसूचना और राज्य में निहित होने का वर्णन करती है। राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने का अधिकार है कि अधिसूचना में वर्णित संपत्ति सभी भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो गई है। इस धारा में आगे कहा गया है कि अधिसूचना में संपदा का विवरण, जैसे कि तौजी संख्या (यदि कोई हो), नाम और मध्यस्थों का पता, शामिल होना चाहिए, जैसा कि कलेक्टर द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है।
उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 4
यह धारा एक समझौते द्वारा संपत्ति के समर्पण का वर्णन करती है। धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले, राज्य सरकार को मध्यस्थों को अपनी संपत्ति के समर्पण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो समर्पण के संबंध में समझौते के निष्पादित होते ही समर्पित संपत्ति सरकार में निहित हो जाएगी। ऐसा प्रस्ताव लिखित रूप में होना चाहिए, और इसमें वे सभी विशिष्ट नियम और शर्तें शामिल होनी चाहिए जिन पर समर्पण किए जाने का प्रस्ताव है।
उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 5
यह धारा, धारा 3 के तहत अधिसूचना जारी करने या धारा 4 के तहत आत्मसमर्पण द्वारा निहित होने के परिणामों का वर्णन करती है। संपूर्ण संपदा, इसके साथ जुड़ी अन्य संपत्तियों सहित, किसी भी भार से मुक्त राज्य में निहित होनी चाहिए, और ऐसे मध्यस्थ जिनकी भूमि निहित की जा रही है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत बचाए गए हितों के अलावा ऐसी संपदा में कोई हित नहीं रखेंगे।
उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 6
यह धारा कुछ ऐसी चीजों का वर्णन करती है जो संपत्ति सरकार में निहित होने के बाद भी बिचौलियों के पास रहती हैं। बिचौलियों को व्यापार, विनिर्माण, वाणिज्य आदि के उद्देश्य से आवासीय या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली गृहस्थी, इमारतें और संरचनाएं रखने की अनुमति है, जैसे गोला, मिल और कारखाने। हालाँकि, आधिकारिक या अन्य संपत्ति उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत सरकार के पास होगी।
उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 7
इस धारा में प्रावधान है कि मध्यस्थ कृषि और बागवानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी भूमि को अपने पास रखने के हकदार होंगे जो निहित होने की तिथि पर उनके खास कब्जे में है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि मध्यस्थों की निजी भूमि, जो उनके अधीन अस्थायी किरायेदार के पास है, सरकार में निहित होगी और अस्थायी किरायेदार को सरकार का किरायेदार माना जाएगा।
उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 की धारा 37
यह धारा सबसे महत्वपूर्ण है और वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा है क्योंकि इसमें मुआवजे के भुगतान के तरीके पर चर्चा की गई है।
इस प्रावधान के तहत कहा गया है कि मुआवजे के आकलन को अंतिम रूप देने के बाद मुआवजा अधिकारी को सूची में उल्लिखित लोगों को मुआवजा देना होगा। मुआवजे का भुगतान करते समय, अधिकारी प्रावधान के विभिन्न खंडों के तहत निर्दिष्ट राशि की कटौती कर सकता है। जब मुआवज़ा एक वार्षिकी हो तो कटौती 35% से अधिक नहीं हो सकती। हालाँकि, यदि ऋण 30 वर्षों में चुकाया नहीं जा सका तो कटौती 50% तक जा सकती है।
इस धारा में आगे यह भी बताया गया है कि यदि मुआवजे का हकदार व्यक्ति मर जाता है, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी ऐसे मुआवजे के हकदार होंगे। मुआवजे पर 2.5% वार्षिक ब्याज मिलता है, जो 30 वार्षिक किश्तों में देय होता है। यदि कानूनी मुद्दों के कारण मुआवजा नहीं चुकाया जाता है, तो ऐसे मुआवजे को राजस्व जमा के रूप में जमा किया जाएगा और एक निर्दिष्ट अवधि के बाद उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। धारा में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि मध्यस्थ, विलेख के माध्यम से, किसी भी प्रकार के भूमि निपटान के लिए कम किराए के रूप में मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमत हो सकते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31
अनुच्छेद 31 वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है क्योंकि इस अनुच्छेद में शुरू में “संपत्ति के अधिकार” को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था। हालाँकि, अधिनियम में राज्य द्वारा सम्पदा के अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
अनुच्छेद 31(4) मुख्य रूप से प्रासंगिक है क्योंकि इसमें कहा गया है कि यदि संविधान के प्रारंभ में किसी विधेयक पर राज्य विधानमंडल में चर्चा की जाती है और यदि वह विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह कानून बन जाता है। ऐसे कानून को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के (2) के विरुद्ध जाने के कारण किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान मामले में विचाराधीन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त थी और इस प्रकार अनुच्छेद 31(4) के तहत संरक्षित किया गया था, लेकिन बाद में एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसे मामले में संबोधित किया गया था।
शुरू में जब भारतीय संविधान बनाया गया था, तब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक था। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत प्रदान किया गया था, जो किसी व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों से संबंधित था, और इस प्रावधान के अनुसार संपत्ति के किसी भी प्रकार के अनिवार्य अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस अनुच्छेद में प्रावधान था कि किसी भी नागरिक को उसकी संपत्ति के स्वामित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। हालाँकि, इस अनुच्छेद के तहत दिए गए अपवादों में से एक यह था कि यदि संपत्ति कानून के अधिकार से अर्जित की जा रही है, तो यह कानूनी रूप से वैध अधिग्रहण होगा। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्जित की जा रही है, तो उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।
हालाँकि, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इस प्रकार, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A तहत एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A
अनुच्छेद 31A इस मामले के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह प्रावधान एक संपत्ति के अधिग्रहण और उससे संबंधित बचत के लिए एक अवसर प्रदान करता है, और वर्तमान मामले में, एक संपत्ति के अधिग्रहण और इसके अलावा, उससे जुड़े मुआवजे के संबंध में सवाल खड़ा हुआ है।
यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) को अपवाद प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस प्रावधान का उद्देश्य जमींदारी और अन्य समान अधिकारों को समाप्त करने वाले कानून की रक्षा और उसे वैध बनाना है। यह अनुच्छेद बताता है कि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी कानून निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है –
- राज्य द्वारा किसी संपत्ति का अधिग्रहण या ऐसे अधिकारों को बदलना या हटाना।
- राज्य द्वारा अंतरिम अवधि के लिए संपत्ति का प्रबंधन अपने हाथ में लेना, या तो सार्वजनिक भलाई के लिए या उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए।
- दो या अधिक निगमों का विलय, या तो सार्वजनिक हित के लिए या बेहतर प्रबंधन के लिए।
- निगमों के प्रबंध एजेंटों, सचिवों, कोषाध्यक्षों, निदेशकों या प्रबंधकों के अधिकारों या शेयरधारकों के मतदान अधिकारों को संशोधित या हटाना।
- खनिजों (मिनरल्स) या खनिज तेलों की खोज या निष्कर्षण से संबंधित किसी समझौते, पट्टे या लाइसेंस के माध्यम से प्राप्त अधिकारों को बदलना या हटाना या ऐसे किसी समझौते, पट्टे या लाइसेंस को समय से पहले समाप्त या रद्द करना।
उपर्युक्त विषय पर बनाए गए कानून शून्य माने जाएंगे यदि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों के साथ असंगत हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि यदि ऐसा कानून राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है, तो इसे कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। आगे कहा गया है कि यदि ऐसे किसी भी कानून में निजी खेती के तहत भूमि के अधिग्रहण की अनुमति है, तो ऐसी भूमि को राज्य द्वारा निश्चित सीमा के भीतर अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है या उस पर कोई इमारत या संरचना कम से कम बाजार मूल्य के मुआवजे का भुगतान किए बिना नहीं बनाई जा सकती है।
के.सी. गजपति नारायण देव बनाम उड़ीसा राज्य (1953) में निर्णय
न्यायालय का मानना था कि यह जांचना आवश्यक है कि “छदमता” के सिद्धांत का वास्तव में क्या अर्थ है। न्यायालय का मानना है कि इस सिद्धांत में विधायिका की ओर से सद्भावना या दुर्भावना का कोई सवाल शामिल नहीं है। पूरा सिद्धांत किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए विधायिका की क्षमता के बारे में सवाल के इर्द-गिर्द घूमता है। न्यायालय ने कहा कि यदि विधायिका किसी कानून को लागू करने में सक्षम है, तो उस स्थिति में, उसे कार्य करने के लिए मजबूर करने वाला मकसद पूरी तरह से अप्रासंगिक है। हालाँकि, अगर बनाया गया कानून ऐसा है कि विधायिका ऐसा कानून पारित करने में सक्षम नहीं है, तो मकसद का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, यह निर्धारित करना कि कोई क़ानून संवैधानिक है या नहीं, हमेशा शक्ति या योग्यता का सवाल होता है। इस विशेष प्रश्न पर, न्यायालय ने अंततः निष्कर्ष निकाला कि मामले का सार महत्वपूर्ण है, और यदि कानून का विषय विधायिका के कानून बनाने की शक्ति से परे है, तो जिस रूप में कानून प्रस्तुत किया जाता है, उसे नकारात्मक रूप से आंका जाने से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए, विधायिका किसी ऐसे काम को पूरा करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का उपयोग नहीं कर सकती जो सीधे नहीं किया जा सकता।
मामले के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों का गंभीरता से विश्लेषण करने और उन पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम की धारा 37, जो 30 वार्षिक समान किस्तों में ब्याज सहित मुआवज़े के भुगतान के बारे में बताती है, राज्य को अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय भुगतान करने की छूट देती है, वह छदम कानून नहीं है। न्यायालय ने इस विशेष निर्णय पर इस तर्क पर भरोसा किया कि यह कानून भारतीय संविधान की अनुसूची VII की सूची III की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत आता है।
न्यायालय का मत था कि यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो उसे इस आधार पर किसी भी हमले से सुरक्षा प्राप्त होती है कि अनुच्छेद 31(2) का अनुपालन नहीं किया गया है। न्यायालय ने पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों में से एक पर कहा कि विधेयक बिना किसी परिवर्तन के पारित किया गया था, और इसलिए अनुच्छेद 31(4) लागू होता है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “ऐसे विधानमंडल द्वारा पारित” अभिव्यक्ति का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत निहित प्रक्रियाओं के अनुसार ““परिवर्तन के साथ या बिना परिवर्तन के पारित” होना चाहिए। इसलिए, यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 31(4) की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और इस आधार पर किसी भी आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रदान किया गया मुआवज़ा अपर्याप्त था। इसके अलावा यह भी निर्णय दिया गया कि राज्य विधानमंडल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(2) के तहत सरकार के प्रबंधन या प्रशासन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भवनों को संपदा के दायरे में रखने का अधिकार है। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इन दलीलों में कोई तथ्य नहीं है, और न्यायालय को इसे खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे खारिज कर दिए गए। हालांकि, मामले में कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न शामिल थे, जिन्हें स्पष्ट किया जाना आवश्यक था, और इसके अलावा, अपील खारिज की जाती है।
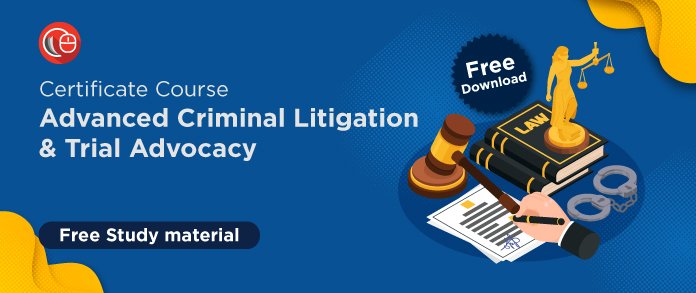
मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय
यूनियन कोलियरी कंपनी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया लिमिटेड बनाम ब्रायडेन (1899)
इस मामले में, ब्रिटिश कोलंबिया कोयला खान विनियमन अधिनियम, 1890 की धारा 4 के बारे में सवाल उठा, जिसमें भूमिगत कोयला कार्य में पूर्ण आयु के चीनी पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह तर्क दिया गया कि ऐसा प्रावधान प्रांतीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वर्तमान प्रश्न का उत्तर न्यायालय ने सकारात्मक तरीके से दिया, और यह निर्णय दिया कि ऐसा निषेध वास्तव में प्रांतीय विधायिका की शक्ति से परे था। आगे कहा गया कि अगर इसे सिर्फ़ कोयला-कार्य विनियमन के रूप में माना जाता है, तो यह निश्चित रूप से ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867 की धारा 92(10) या धारा 92(13) के अंतर्गत आ सकता है। हालाँकि, चूँकि विचाराधीन मौजूदा प्रावधान विशेष रूप से चीनी पुरुषों को लक्षित करता है, इसलिए यह अधिनियम की धारा 91(25) के अंतर्गत आता है, जो संघीय संसद का विशेष अधिकार क्षेत्र है। इसके बाद, न्यायिक समिति द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ब्रिटिश कोलंबिया कोयला खान विनियमन अधिनियम, 1890 वास्तव में कोयला खदान सुरक्षा के बारे में नहीं था, बल्कि इसके बजाय, यह चीनी लोगों के साथ भेदभाव करने का एक तरीका था।
बिहार राज्य बनाम महाराजा कामेश्वर सिंह एवं अन्य (1952)
इस मामले में, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उन्हें मुआवजा देने के उद्देश्य से ज़मींदारों का वर्गीकरण किया गया था। यह तर्क दिया गया कि ऐसा वर्गीकरण भेदभावपूर्ण है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत कानून के समान संरक्षण से इनकार करता है। परिणामस्वरूप, बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(b) और धारा 23(f) नामक दो प्रावधानों को इस आधार पर असंवैधानिक माना गया कि ये प्रावधान संविधान के साथ धोखाधड़ी करते हैं। वर्तमान मामले में न्यायालय ने देखा कि हालाँकि अधिनियम के कुछ प्रावधान ज़मींदारों के खिलाफ़ कठोर और बुरे हैं, लेकिन वे पूरे अधिनियम को संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं बनाते हैं।
ओंटारियो के अटॉर्नी-जनरल बनाम पारस्परिक बीमाकर्ता और अन्य (1924)
इस मामले में, न्यायमूर्ति डफ द्वारा यह राय व्यक्त की गई थी कि यदि कानून बनाने का प्राधिकार सीमित या योग्य प्रकृति का है, तो उन परिस्थितियों में, ऐसे कानून के सार की कठोरता से जांच करना आवश्यक हो सकता है, ताकि यह स्पष्ट रूप से समझा जा सके कि विधायिका वास्तव में क्या कर रही है।

निष्कर्ष
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अपने निर्णय के माध्यम से यह प्रदर्शित किया है कि विचाराधीन अधिनियम महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है और भारत में भूमि सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मामले ने सरकार की उस प्रतिबद्धता को उजागर किया है जिसके तहत वह स्थायी ज़मींदारी व्यवस्था को समाप्त करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि जो लोग वास्तविक कृषक या किरायेदार हैं, उन्हें अधिनियम के माध्यम से लाभ मिले। अधिनियम की असंवैधानिकता के बारे में भूमिधारक की चुनौती को बरकरार नहीं रखा जा सका, और न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य विधानमंडल ऐसे कानून बनाने के लिए सक्षम है और संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।
इसलिए, मुआवज़े के मामले में लगातार बने रहने वाले प्रमुख मुद्दे को सुलझा लिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि राज्य के पास इस तरह के सुधारों को लागू करने का अधिकार है और मुआवज़े के भुगतान के तरीके निष्पक्ष और कानूनी रूप से वैध हैं। हालाँकि, न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि कुछ संवैधानिक प्रश्न हैं जिन्हें वर्तमान मामले में संबोधित करने की आवश्यकता है, लेकिन केवल इस आधार पर कि अधिनियम को भारतीय संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जा सकता है। यह मामला गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग का समर्थन करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उड़ीसा में जमींदारी प्रथा पर इस निर्णय का क्या प्रभाव होगा?
उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1952 को कानूनी रूप से वैध मानने के बाद, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और इस प्रकार, किसानों और किरायेदारों को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से भारी लाभ हुआ, जो भूमि वितरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उपस्थित मुद्दों के संबंध में संपत्ति के अधिकार की व्याख्या किस प्रकार की?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मत था कि, यद्यपि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है। फिर भी, इसके साथ ही, सरकार के पास सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कुछ संपत्ति अर्जित करने की शक्ति है, और इस तरह के अधिग्रहण के लिए उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, जो वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 37 के अनुसार दिया गया था।
वर्तमान मामले में बिहार राज्य बनाम महाराजा कामेश्वर सिंह एवं अन्य में दिए गए निर्णय की प्रासंगिकता क्या है?
बिहार राज्य बनाम महाराजा कामेश्वर सिंह एवं अन्य, वर्तमान मामले में संदर्भित मामलों में से एक है और इसने मामले के निर्णय को आकार देने में मदद की है, क्योंकि इसमें भूमि सुधारों की संवैधानिक वैधता और मुआवजे से संबंधित मुद्दों जैसे समान प्रश्न शामिल हैं।
संदर्भ
- भारतीय संवैधानिक कानून एम.पी. जैन द्वारा







