यह लेख Shweta Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णय का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इसके अलावा, इसमें आज के परिदृश्य में इस मामले की प्रासंगिकता और महत्व पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्तिगत विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। हालाँकि, भाग III के तहत प्रदान किए गए कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं हैं। इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तिगत अधिकारों के प्रवर्तन से आम जनता के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और आम जनता के अधिकारों के बीच सीधा विरोधाभास होता है। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है: व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के व्यापक हितों की रक्षा करते हुए इस तरह के संघर्ष को कुशलतापूर्वक कैसे हल किया जा सकता है? करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) (जिसे आगे “मामला” कहा जाएगा) का मामला इस प्रश्न से उपयुक्त रूप से निपटता है। यह मामला विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और संविधान के तहत अभियुक्तों को प्रदान की गई प्रक्रियात्मक सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बड़े पैमाने पर जनता का कल्याण और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता भी सुरक्षित रहे।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) का संक्षिप्त विवरण
मामले का नाम
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994)
फैसले की तारीख
11 मार्च, 1994
मामले के पक्षकार
याचिकाकर्ता
करतार सिंह
प्रतिवादी
पंजाब राज्य
प्रस्तुतकर्ता
याचिकाकर्ता
श्री बलवंत सिंह मलिक, श्री राम जेठमलानी और श्री हरदेव सिंह।
प्रतिवादी
श्री के.टी.एस. तुलसी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
समतुल्य उद्धरण
1994 एससीसी (3) 569, जेटी 1994 (2) 423,1994 स्केल 1.
मामले के प्रकार
रिट याचिका संख्या 1833/1984 और रिट याचिका (क्रि.) संख्या 194/1989।
न्यायपीठ
न्यायमूर्ति आर.एम. सहाय, न्यायमूर्ति एस.आर. पांडियन, न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी, न्यायमूर्ति के. रामास्वामी और न्यायमूर्ति एस.सी.अग्रवाल।
निर्णय के लेखक
मुख्य निर्णय न्यायमूर्ति आर.एम. सहाय द्वारा लिखा गया था तथा असहमतिपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ति के. रामास्वामी द्वारा लिखा गया था।

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) की पृष्ठभूमि
यह 1980 का दशक था जब भारत अनेक आतंकवादी हमलों, अशांति, गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं से ग्रस्त था। ऐसी गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पंजाब राज्य था। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियां देखी गईं जिनमें बड़े पैमाने पर हत्याएं और आगजनी के हमले शामिल थे। कुछ ही समय में ये गतिविधियां अन्य पड़ोसी राज्यों में भी फैल गईं और सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं रहीं। ये गतिविधियां जिन पड़ोसी राज्यों में फैलीं, वे थे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जिससे पूरे देश में अस्थिरता और भय बढ़ गया। इस दौरान कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और तीव्र विस्फोटकों के कारण कई सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। इससे आम जनता में भय की भावना पैदा हुई और सांप्रदायिक शांति एवं सद्भाव बाधित हुआ। इस संकट से निपटने के लिए, केंद्र सरकार ने दो कानून पारित किए, अर्थात्, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985, और इसकी समाप्ति के बाद आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987। ये कानून आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने के उद्देश्य से पारित किये गये थे। ये दोनों कानून पूरे क्षेत्र में हो रही आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए बनाए गए थे। आतंकवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने और इन गतिविधियों में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए, अधिनियमों में दो अपराध शामिल किए गए हैं, अर्थात् “आतंकवादी कृत्य” और “विघटनकारी गतिविधियाँ”। इन अधिनियमों में आतंकवादी गतिविधियों में आए बदलाव और विकास को मान्यता दी गई है, जो खतरनाक रूप ले चुके हैं, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अधिनियमों की प्रस्तावना में विघटनकारी गतिविधियों में खतरनाक वृद्धि की गंभीरता और समीचीनता को रेखांकित किया गया है।
इन कानूनों के प्रावधान कठोर प्रकृति के होने के कारण, विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी आलोचना की गई थी, और इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने इन अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि यह भारतीय संविधान के भाग III के तहत निहित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) के तथ्य
वर्तमान मामले में, रिट याचिका, आपराधिक अपील और विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के रूप में कई कानूनी कार्यवाहियाँ दायर की गईं। इन मामलों में एक समान आधार था। सभी मामले तीन विधायी अधिनियमों की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर किए गए थे, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम (1984 अधिनियम), आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (1985 अधिनियम), और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (1987 अधिनियम) को सामूहिक रूप से “आलोचना योग्य अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया जाता है, 1985 और 1987 के अधिनियमों को आमतौर पर टाडा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, इस मामले के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता (यू.पी. संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 अधिनियम) की धारा 9 की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई। 1976 अधिनियम की धारा 9 के कार्यान्वयन के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता (1973 संहिता) की धारा 438 के आवेदन पर रोक लगा दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने मामलों की सुनवाई करते हुए इन मुद्दों को एकत्रित किया तथा 1984 अधिनियम, 1985 अधिनियम, 1987 अधिनियम तथा 1976 अधिनियम की धारा 9 की वैधता पर साझा निर्णय सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मामले का निर्णय इन तीनों अधिनियमों की वैधता पर निर्णय के आधार पर अलग-अलग किया जाएगा।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) के कानूनी पहलू
मामले के विवरण में जाने से पहले, विभिन्न कानूनी पहलुओं की मूल बातें समझना महत्वपूर्ण है, जो संबंधित पक्षों और अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को बेहतर ढंग से समझने के लिए शामिल हैं और जिन पर संबंधित पक्ष और अदालत भरोसा करते हैं।
संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति का वितरण
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण भारत की संघीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं को परिभाषित करता है। विधायी शक्ति वह प्राधिकार है जो संघ और राज्य दोनों में कानून बनाने, संशोधित करने और लागू करने के लिए निहित है। यह कानून किसी क्षेत्र में असामान्य मुद्दों या अराजकता से निपटने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए समाज में व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक कुशल तंत्र है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार के दोनों स्तरों पर कानूनों का निर्माण और उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 245-254 के तहत संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया है।
भारत में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण मूलतः भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत स्थापित किया गया था, जिसे बाद में भारतीय संविधान के तहत शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य की विधायी शक्ति को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला अनुच्छेद 245 के तहत प्रदत्त क्षेत्र से संबंधित है और दूसरा विधान के विषय-वस्तु से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत तीन सूचियों में विभाजित किया गया है।
अनुच्छेद 245 संघ और राज्य द्वारा विधायी शक्ति के प्रयोग की क्षेत्रीय सीमाओं को रेखांकित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, संघ को संपूर्ण राष्ट्र या भारत के राज्यक्षेत्र के कुछ भागों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी ओर, अलग-अलग राज्य विधानमंडल केवल अपने-अपने राज्यों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में ही कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 245 संघ द्वारा अधिनियमित कानूनों के राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है। यह कुछ मामलों में संसद की सर्वोच्चता तथा ऐसे विषयों पर कानून बनाने के उसके अधिकार पर बल देता है जिनका प्रभाव राष्ट्रीय क्षेत्र से परे भी हो सकता है। इसमें प्रावधान है कि संघ द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वे भारत के प्रादेशिक सीमा से बाहर लागू होते हैं या उन क्षेत्रों पर प्रभावी हैं जो भारत की प्रादेशिक सीमा से बाहर हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 ने सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियाँ बनाकर संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति वितरित की है, अर्थात् संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
इस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार, केवल संघ सरकार को संघ सूची (सूची I) के अंतर्गत निहित 97 प्रविष्टियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। जहां तक राज्य सूची (सूची II) का संबंध है, अनुच्छेद 246 के खंड (3) में प्रावधान है कि केवल राज्य ही उक्त सूची के अंतर्गत उल्लिखित 66 मदों के लिए कानून बना सकता है। समवर्ती सूची (सूची III) के संबंध में, जिसमें 47 प्रविष्टियाँ हैं, संघ और राज्य दोनों ही इसमें निहित मदों से संबंधित कानून बना सकते हैं।
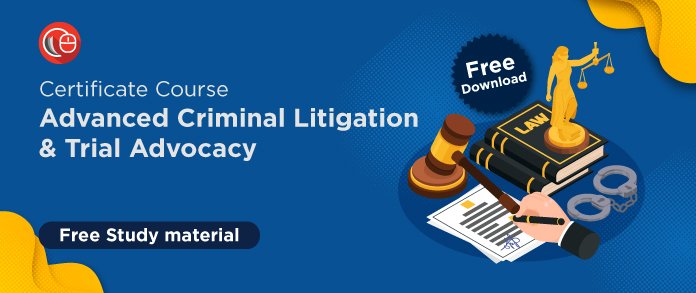
अनुच्छेद 248 और सूची 1 की प्रविष्टि 97 के संचयी पठन (कम्युलेटिव रीडिंग) से अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार को सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में सूचीबद्ध न किए गए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। एक अन्य अनुच्छेद जो संघ द्वारा निर्मित विधायिका की प्रधानता की अनुमति देता है, वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254 है। यह अनुच्छेद संघ द्वारा बनाए गए कानूनों को संघ और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच उत्पन्न किसी भी संघर्ष की स्थिति में अधिभावी प्रभाव प्रदान करता है, भले ही वह कानून राज्य विधान से पहले बनाया गया हो या बाद में बनाया गया हो। राज्य द्वारा बनाए गए कानून केवल एक ही स्थिति में लागू होंगे, अर्थात, यह तब लागू होगा जब केंद्र सरकार ने कानून बनाया हो और ऐसे कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई हो।
उपर्युक्त अनुच्छेदों का तात्पर्य यह है कि संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति का वितरण सही नहीं है और भारतीय संविधान के तहत तीन सूचियों में प्रगणित विषयों के भीतर अतिव्यापन (ओवरलैपिंग) के उदाहरण हैं। इसलिए, ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धांत स्थापित किए हैं जिनका उपयोग विधायी सूची में प्रविष्टियों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) के मामले में, भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त तीन सूचियों की प्रविष्टियों की व्याख्या करते समय दृष्टिकोण पर चर्चा की गई थी। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि संकीर्ण और कठोर दृष्टिकोण के बजाय व्यापक और लचीला दृष्टिकोण कैसे अपनाया जाए। न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए कि विभिन्न सूचियों में या एक ही सूची में प्रविष्टियों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है, न्यायालय की यह जिम्मेदारी रेखांकित की कि वह इन प्रविष्टियों के पीछे के वास्तविक इरादे और उद्देश्य को समझे, तथा ऐसे टकराव को दूर करे। इस जिम्मेदारी में संबंधित कानून का विश्लेषण करना और कानून का सार-तत्व ज्ञात करना शामिल है। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह पता लगाना है कि क्या यह संघ या राज्य सरकारों को आवंटित विषयों के साथ अधिक निकटता से संरेखित है।
सार और तत्व का सिद्धांत
सार और तत्व का सिद्धांत तब अपनी भूमिका निभाता है जब इस बात पर संदेह होता है कि किसी विशेष विधायिका (संघ या राज्य) के पास कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है। ऐसा संदेह तब होता है जब एक सूची में शामिल विषय-वस्तु से संबंधित कानून किसी अन्य सूची में शामिल विषय-वस्तु को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में कानून का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य, उसका “वास्तविक उद्देश्य” अर्थात् कानून का सार और तत्व जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें यह समझना शामिल है कि कानून वास्तव में क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड (1947) के मामले में, लॉर्ड पोर्टर ने प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पक्ष में बोलते हुए कहा कि विधायी व्यवहार में यह अक्सर होता है कि मुख्य रूप से एक सूची में मौजूद विषय-वस्तु पर बनाया गया कानून, किसी अन्य सूची में मौजूद विषय-वस्तु को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों की कठोर शाब्दिक व्याख्या अव्यावहारिक होगी क्योंकि इससे विधायी अक्षमता के आधार पर कई क़ानून अमान्य हो जाएंगे। इस समस्या से बचने के लिए, भारतीय न्यायपालिका न्यायिक समिति द्वारा विकसित सिद्धांत को अपनाकर, अधिनियम केसार और तत्व की जांच करने का कार्य करती है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या यह कानून किसी विधायी सूची के दायरे में आने वाले विषयों से संबंधित है या नहीं।
संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र सुनवाई
शीघ्र सुनवाई का अधिकार एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है, जो उत्पीड़न के एक रूप के रूप में गैरकानूनी कारावास को रोकने के लिए एक अद्वितीय उपाय है। लम्बे समय तक कारावास से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने के अलावा, यह चिंता और परेशानी की भावना को भी कम करता है, जो आमतौर पर आपराधिक मामले से जुड़ी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि न्याय कुशल और बिना किसी अनावश्यक देरी के होना चाहिए। शीघ्र सुनवाई से झूठे आरोप लगाए गए व्यक्ति के लिए अच्छा बचाव स्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। लेकिन व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की तात्कालिकता के अलावा, मुकदमों में तेजी लाने की सामाजिक आवश्यकता भी है। शीघ्र न्याय निर्णय प्रक्रिया न केवल न्याय की गारंटी देती है, बल्कि न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए, यह न्यायिक प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में से एक है जो इसकी अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही इस बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है कि न्याय में देरी वास्तव में न्याय से इनकार है।
शीघ्र सुनवाई का विचार न केवल कानून का शासन है, बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की भावना का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संबंध में, इस अधिकार की मौलिक प्रकृति केवल शारीरिक स्वतंत्रता की मांग करने से आगे बढ़कर कानूनी कार्यवाही के प्रत्येक चरण में न्याय की शीघ्रता को भी शामिल करती है। प्रारंभिक गिरफ्तारी और हिरासत से लेकर, शीघ्र सुनवाई के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, तथा इसे कानूनी प्रक्रिया के सभी चरणों जैसे जांच, पूछताछ, परीक्षण और अपील में बनाए रखा जाता है।
शीघ्र सुनवाई के सिद्धांत के इस विस्तृत अनुप्रयोग का उद्देश्य किसी भी पूर्वाग्रह को रोकना है, जो अपराध के घटित होने और कार्यवाही के समापन के बीच अनुचित और अनावश्यक देरी के कारण उत्पन्न हो सकता है।
हुसैनारा खातून (1) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य (1980) के मामले में, अनुच्छेद 21 पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रक्रिया उचित समय के भीतर सुनवाई की गारंटी नहीं देती है, उसे “उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत” के बराबर नहीं माना जा सकता है और यदि ऐसा है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। फैसले में अदालत ने दोहराया कि मुकदमे के मानक के रूप में शीघ्र और समयबद्ध सुनवाई अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य घटक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1987) और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस.नायक (1991) जैसे मामलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि संविधान में निहित अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्निहित घटक के रूप में त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए। इसलिए, कानूनी ढांचे में ऐसी प्रक्रिया स्थापित की जानी चाहिए जो न केवल तर्कसंगत हो बल्कि न्यायसंगत और निष्पक्ष भी हो, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हो कि किसी व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के समय पर न्याय मिले।
संस्वीकृति
भारतीय संविधान के साथ-साथ प्रक्रियात्मक कानून और साक्ष्य से संबंधित कानून में आपराधिक मामले में व्यक्तिगत आरोपी के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए एक अंतर्निहित तंत्र मौजूद है। इस तरह की व्यवस्था का आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में निहित है, जिसके अनुसार किसी अपराध के आरोपी और आपराधिक कार्यवाही में शामिल किसी भी व्यक्ति को ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया जाएगा जो उसकी स्थिति के लिए प्रतिकूल हो या जिसके कारण उसे दोषसिद्धि हो सकती हो।
अनुच्छेद 20(3) का मसौदा ब्रिटिश आपराधिक न्यायशास्त्र प्रणाली में निहित सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया था। ऐसे सिद्धांतों को अमेरिकी प्रणाली द्वारा भी अपनाया गया है तथा संघीय अधिनियमों में भी इन्हें शामिल किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पांचवें संशोधन में भी इसी प्रकार की भावना व्यक्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि मामले में फंसाए गए व्यक्ति को किसी भी आपराधिक कार्यवाही में स्वयं को दोषी ठहराने के लिए मजबूर किया जाएगा।
भारत में, इस सिद्धांत को विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त है। मूलतः, अनुच्छेद 20(3) यह गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य किए जाने से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे हमारी आपराधिक न्याय प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित होती है।
1973 संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (साक्ष्य अधिनियम) में विभिन्न वैधानिक प्रावधान निहित हैं, इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 22 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

1973 की संहिता की धारा 164 में निहित प्रावधानों के माध्यम से कानून के तहत ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्ति द्वारा किए गए बयानों और संस्वीकृति को रिकार्ड करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। ये सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करते हैं कि संस्वीकृति और बयान दर्ज करते समय कानूनी औपचारिकताओं और वैधानिक शर्तों का विधिवत पालन किया जाए, जिसमें धारा 164 की उप-धारा (2) से (6) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न करना भी शामिल है।
पिछली संहिता के अंतर्गत, धारा 164 की उपधारा (1) में पुलिस अधिकारियों को जांच के दौरान कोई भी बयान या स्वीकारोक्ति दर्ज करने से स्पष्ट रूप से रोक दिया गया था। 1973 संहिता जांच प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए उपधारा (1) में एक अतिरिक्त प्रावधान स्थापित करती है। इस प्रावधान के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया संस्वीकृति किसी निरीक्षक द्वारा दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, जिसके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हों। यद्यपि 1973 की संहिता में प्रावधान जोड़ना पुरानी संहिता की धारा 164(1) के मुख्य उद्देश्य में एक अतिरिक्त प्रावधान है, फिर भी यह मूल संदेश को बरकरार रखता है।
साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच और आपराधिक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन न हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और 26, पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई संस्वीकृति को बयान देने वाले व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करने पर प्रतिबंध लगाती है। हालाँकि, धारा 27 इस नियम में अपवाद की अनुमति देती है। इस धारा के अनुसार, हिरासत में लिए गए अभियुक्त से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जा सकता है, यदि इससे मामले से संबंधित तथ्यों का पता चलता हो। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण धारा, जो अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृति से भी संबंधित है, वह है साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 और धारा 30। धारा 24 के अनुसार आपराधिक कार्यवाही में किसी अभियुक्त से प्रलोभन, धमकी या वादे के माध्यम से प्राप्त की गई संस्वीकृति अप्रासंगिक माने जाएंगे। दूसरी ओर, धारा 30 में यह प्रावधान है कि यदि एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई संस्वीकृति, जिसमें वह स्वयं तथा उसी मामले में संयुक्त रूप से विचारित अन्य व्यक्ति शामिल हैं, साबित हो जाता है, तो न्यायालय ऐसी संस्वीकृति पर अन्य व्यक्तियों तथा संस्वीकृति बयान देने वाले दोनों के विरुद्ध विचार कर सकता है।
इस प्रकार, 1973 संहिता और साक्ष्य अधिनियम के तहत निहित प्रावधान बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत के साथ, अभियुक्तों के प्रति राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षात्मक तंत्र की रूपरेखा तैयार करते हैं। परिणामस्वरूप, हिरासत में रहते हुए किसी अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष दी गई संस्वीकृति का इस्तेमाल मामले में शामिल व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया जा सकता।
1973 संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत
1973 संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अदालत में पेश होने से पहले जमानत प्राप्त कर सकता है। इस कानूनी व्यवस्था के माध्यम से, कोई भी नागरिक किसी अपराध का अभियुक्त घोषित होने या उस पर अपराध करने का आरोप लगने से पहले ही जमानत मांगकर मामले को सक्रिय रूप से उठा सकता है। अग्रिम जमानत उन व्यक्तियों के लिए एहतियाती उपाय के रूप में सामने आती है, जो पेशेवर या व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण गलत तरीके से अपराध या आरोप लगाए जाने से डरते हैं। यह अन्यथा साबित होने तक उनकी निर्दोषता को सुरक्षित रखता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की रक्षा होती है।
अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता को संबंधित राज्य के सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करना आवश्यक है। आवेदन पत्र भर दिए जाने के बाद न्यायालय आवेदन पत्र की जांच करता है तथा मामले की प्रकृति और निर्णय लेने की शर्तों सहित विभिन्न कारकों का आकलन करता है। यदि अग्रिम जमानत मंजूर हो जाती है तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद रिहाई मिल जाती है। जमानत देने से पहले अदालत धारा 438 के तहत प्रदत्त कई शर्तों पर विचार करती है जिनमें शामिल हैं:
- आवश्यकता पड़ने पर पुलिस पूछताछ में सहयोग करने की याचिकाकर्ता की क्षमता;
- मामले से जुड़े लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने पर प्रतिबन्ध, जैसे कि धमकी, रिश्वत, या उनकी गवाही को प्रभावित करने या कानून प्रवर्तन से कुछ जानकारी छिपाने का वादा, तथा
- याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया गया कि उसे भारत नहीं छोड़ना चाहिए तथा छोड़ने का प्रयास करने से पहले न्यायालय की अनुमति लेनी चाहिए।
ये शर्तें अभियुक्तों की सुरक्षा और न्याय के हितों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं, जिससे निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित हो सके और धारा के किसी भी दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) में उठाए गए मुद्दे
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या टाडा अधिनियम ‘लोक व्यवस्था’ से संबंधित सूची II की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत आते हैं।
- क्या 1984 का अधिनियम केन्द्र सरकार की ओर से विधायी क्षमता की कमी के कारण अधिकार-विहीन है।
- क्या आरोपित अधिनियम सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारतीय संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
- क्या पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।
- क्या 1973 संहिता की धारा 438 को अप्रभावी बनाने वाला प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है और क्या विधानमंडल के पास इसकी प्रयोज्यता को हटाने की क्षमता है।
- क्या 1973 संहिता की धारा 437(3) में निहित सीमाओं के अतिरिक्त जमानत देने पर गंभीर सीमाएं लगाना उचित और न्यायोचित है।
- क्या अनुच्छेद 226 के तहत जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय में जाने के व्यक्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है, जहां अपराध 1987 के अधिनियमों के अंतर्गत आता है।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) में पक्षों की दलीलें
इस मामले में उठाए गए मुद्दों के पक्ष और विपक्ष में पक्षों द्वारा कई तर्क दिए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री बलवंत सिंह मलिक, श्री राम जेठमलानी और श्री हरदेव सिंह ने दलीलें पेश कीं। दूसरी ओर, तत्कालीन विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के.टी.एस. तुलसी ने प्रतिवादियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया।
याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्क
याचिकाकर्ताओं ने पूरे जोर-शोर से उक्त अधिनियम की संवैधानिक वैधता के विरुद्ध अनेक तर्क प्रस्तुत किए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने तर्क दिया कि इन विवादित अधिनियमों को पारित करके केन्द्रीय विधानमंडल अपनी शक्तियों से आगे चला गया है तथा इसकी विधायी क्षमताओं की वैधता पर सवाल उठाया है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि 1987 के अधिनियम की धारा 3, 4, 8, 9, 15, 20 (3), 22 जैसे कुछ प्रावधान संविधान के भाग III में निहित मूल अधिकारों के खिलाफ हैं और इस प्रकार, उनकी वैधता के संदर्भ में संदिग्ध हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने सार्वभौमिक मानवाधिकार सिद्धांतों और मानवीय कानून के प्रति पूर्वाग्रह के लिए अधिनियमों की निंदा की, तथा न्याय और निष्पक्षता के बुनियादी मानकों को बनाए रखने में उनकी पक्षपातपूर्ण और विफलता पर जोर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इन अधिनियमों की निंदा करते हुए इन्हें क्रूर और निंदनीय बताया तथा कहा कि ये बर्बर हैं, साथ ही इनमें कमजोर पड़ने और दुरुपयोग की भी संभावना है, जो कि इनका अंतर्निहित स्वभाव है। उन्होंने इस आधार पर भी उक्त अधिनियमों को चुनौती दी कि पुलिस बलों को अपार शक्ति प्राप्त है, जिसमें न्यायालय में पुलिस द्वारा दर्ज की गई संस्वीकृति की स्वीकार्यता भी शामिल है। वे इस शक्ति का दुरुपयोग निर्दोष नागरिकों के खिलाफ ‘जासूसी अभियान’ चलाकर करेंगे, जिससे भय का माहौल पैदा होगा, जो संस्थागत आतंक से चिह्नित ऐतिहासिक युगों को दर्शाता है। अपने तर्कों की विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि विचाराधीन अधिनियम न केवल संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि प्राकृतिक न्याय और मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों से भी विचलित हैं।

प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए तर्क
प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के तर्कों का विरोध करते हुए उक्त अधिनियमों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि यह मनमाना है तथा कानून के शासन के विरुद्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि आतंकवादियों की क्रूर और विघटनकारी गतिविधियों से देश के मूल मूल्यों का उल्लंघन किए बिना कड़े कानूनों को लागू करके ही प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। परिणामस्वरूप, उन्होंने सुझाव दिया कि इन कार्रवाइयों के लिए वैधानिक ढांचे की सीमाओं के भीतर आतंकवाद से लड़ने के लिए राज्य की कानूनी शक्तियों को बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। इन विवादित अधिनियमों को पारित करने के लिए एक विस्तृत संसदीय प्रक्रिया का पालन किया गया, तथा विधायिका की इस राय को लागू किया गया कि आतंकवादी और अव्यवस्थित गतिविधियों में भारी वृद्धि के कारण मौजूदा आपराधिक कानूनों की कमियों को पूरा करने के लिए ये बहुत आवश्यक थे। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियमों की जांच से न तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन प्रदर्शित होता है और न ही विधायी योग्यता का अभाव। उन्होंने तर्क दिया कि इन अधिनियमों को उचित प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य से बनाया गया था।
इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि आतंकवादी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्रूर और बर्बर से लेकर अमानवीय तक विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन रणनीतियों में नागरिकों को आतंकित करना और उन्हें निराश और असहाय महसूस कराने, लक्षित देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, तथा सहानुभूति या प्रचार पाने के लिए सरकार की अत्यधिक प्रतिक्रिया का लाभ उठाना शामिल था। उत्तरदाताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन आतंकवादी गतिविधियों के मुख्य पीड़ित निर्दोष व्यक्तियों के समूह हैं, जिन्हें आतंकवादी समूहों द्वारा मीडिया कवरेज को अधिकतम करने और आतंकवादियों के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए चुना जाता है। इसलिए, इन विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इन विवादित अधिनियमों को लागू करना आवश्यक था, तथा राष्ट्रीय मूल्यों और कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये विवादित अधिनियम भारतीय संविधान के भाग III के तहत निहित किसी भी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं और कानूनी प्रक्रिया और प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) में निर्णय
अधिकांश न्यायाधीशों ने विवादित अधिनियमों अर्थात् 1984 अधिनियम, 1985 अधिनियम और 1987 अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि राज्य और संघ सरकार के बीच, संघ सरकार ही उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए सक्षम है, क्योंकि ये अधिनियम गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था से निपटते हैं, जो सूची I की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत संघ की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। न्यायालय ने आगे कहा कि विधायिका को किसी विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए विशेष कानून बनाने तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने का पूर्ण अधिकार है। आतंकवाद एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बाधित करने की प्रवृत्ति है, इसलिए विधायिका को समाज पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए एक विशिष्ट कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए, विवादित अधिनियम विशेष विधान हैं, जिनमें आपराधिक कार्यवाही के प्रक्रियात्मक पहलू को शामिल करने वाले विशेष प्रावधान जैसे कि संस्वीकृति दर्ज करना, विशेष अदालतों की स्थापना करना, तथा जमानत प्रदान करना आदि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 20 तथा 21 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के विरुद्ध है।
विवादित अधिनियमों की वैधता पर अपना निर्णय पूरा करने के लिए, न्यायालय ने विभिन्न मुद्दे तैयार किए तथा पक्षों द्वारा उठाए गए विवादों का पूर्णतः निपटारा करने के लिए प्रत्येक मुद्दे पर अपना निर्णय दिया। इसलिए, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए न्यायालय के मुद्देवार निर्णय पर गौर करना आवश्यक है।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) में मुद्दावार निर्णय
क्या टाडा अधिनियम ‘लोक व्यवस्था’ से संबंधित सूची II की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत आते हैं?
अदालत ने इस मुद्दे पर दो अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाकर अपना निर्णय दिया। प्रारंभ में, इसने सार्वजनिक व्यवस्था के अर्थ और अवधारणा का गहन विश्लेषण किया। इसके बाद, न्यायालय ने चुनौती दिए गए कानून के सार को सुनिश्चित करने के लिएसार और तत्व के सिद्धांत को लागू किया।
याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर कि टाडा अधिनियम, विशेष रूप से 1987 अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था के विषय-वस्तु से संबंधित है, जो प्रविष्टि 1 सूची II के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ से संबंधित अवधारणा की व्याख्या की। अदालत ने कहा कि भारतीय कानून के तहत अव्यवस्था के विभिन्न स्तर माने गए हैं। राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (1965) मामले में की गई टिप्पणी को उद्धृत करते हुए, अदालत ने माना कि इन स्तरों को तीन मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है: कानून और व्यवस्था, “सार्वजनिक व्यवस्था,” और “राज्य की सुरक्षा।” “कानून और व्यवस्था” में कम गंभीर सभी गड़बड़ियां शामिल हैं, जबकि “सार्वजनिक व्यवस्था” में अधिक गंभीर गड़बड़ियां शामिल हैं, तथा “राज्य की सुरक्षा” में सबसे गंभीर गड़बड़ियां शामिल हैं।
न्यायालय ने अनुच्छेद 245(1) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, जो राज्य विधानमंडल को अपने-अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, तथा कानून के विषय के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे को ध्यान में रखते हुए कहा कि सूची II की प्रविष्टि 1 के तहत सार्वजनिक व्यवस्था शब्द का अर्थ राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर शांति को प्रभावित करने वाली कम गंभीर अव्यवस्था है। परिणामस्वरूप, राष्ट्र की समग्र सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाली गंभीर प्रकृति की अव्यवस्था “सार्वजनिक व्यवस्था” के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि गंभीर प्रकृति की गड़बड़ियों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। भारत की रक्षा से संबंधित सूची I की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खतरा पूरी तरह से प्रविष्टि 1 के दायरे में नहीं आता हो, फिर भी संघ अनुच्छेद 248 के तहत अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग करके कानून बना सकता है। सूची I की प्रविष्टि 97 के अंतर्गत, संघ को तीनों सूचियों में से किसी में भी सूचीबद्ध न किये गये विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। अदालत ने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता तभी सफल हो सकते हैं, जब वे यह प्रदर्शित कर दें कि चुनौती दिया गया अधिनियम केवल एक राज्य के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित है, जो राज्य की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है।
इस मुद्दे पर निर्णय तक पहुंचने में स्वयं की सहायता करने के लिए, न्यायालय ने विचाराधीन कानून की वास्तविक प्रकृति की व्याख्या करने के लिए सार और सार के सिद्धांत को लागू किया। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में 1987 के अधिनियम के सार और सार को समझने के लिए, इसकी प्रस्तावना, उद्देश्यों और तर्कों के विवरण, इसके महत्व और कानून के उद्देश्य तथा टाडा अधिनियम के उद्देश्यों के साथ इसके दायरे और संबंध की जांच विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। अदालत ने गंभीर और क्रूर गतिविधियों की श्रृंखला और उन्हें अंजाम देने के तरीके का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला कि आतंकवादियों द्वारा की गई इस तरह की हिंसा और व्यवधान भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, चाहे यह विदेशी देशों द्वारा हमलों के कारण हो या भारत के भीतर हिंसा के कारण हो।

वर्तमान मामले में सार और तत्व के सिद्धांत के अनुप्रयोग का पता लगाने के बाद, अदालत ने माना कि विवादित अधिनियम मुख्य रूप से टाडा अधिनियमों को संघ द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिए अधिनियमित किया गया है और आतंकवाद शब्द को स्थानीय क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाली गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद द्वारा अंजाम दी जाने वाली गतिविधियां या तो बाहरी ताकतों की ओर से या राष्ट्र-विरोधी तत्वों की ओर से राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली बहुत अधिक गंभीर स्थिति है। प्रस्तावना में “आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों” शब्दों का प्रयोग स्वयं स्पष्ट करता है कि टाडा अधिनियमों को उन गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालती हैं, साथ ही ऐसी गतिविधियों को भी रोका गया है जो भारत के किसी हिस्से के अधिग्रहण या संघ से भारत के किसी हिस्से के अलगाव को बढ़ावा देती हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने श्री जेठमलानी द्वारा की गई इस दलील को खारिज कर दिया कि 1987 के अधिनियम की प्रस्तावना में आतंकवादी गतिविधियों की कल्पना की गई है, जो सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का एक गंभीर रूप मात्र है, तथा यह अकल्पनीय और अस्वीकार्य है।
इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों से न्यायालय ने माना कि चुनौती दिए गए अधिनियम सूची I की प्रविष्टि 1, अर्थात् ‘भारत की रक्षा’ के अनुसार संघ की विधायी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। संघ को सूची I की प्रविष्टि 97 के साथ अनुच्छेद 248 के अंतर्गत टाडा अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।
क्या 1984 का अधिनियम केन्द्र सरकार की विधायी क्षमता की कमी के कारण अधिकार-विहीन है?
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1984 के अधिनियम की वैधता को चुनौती टाडा अधिनियम के समान ही आधार पर दी गई थी। श्री हरदेव सिंह ने तर्क दिया था कि 1984 का अधिनियम केंद्र सरकार की विधायी क्षमता से बाहर था, क्योंकि अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मुद्दे से निपटता था, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा निपटाया जाना था। उपर्युक्त तर्क के महत्व को जानने के लिए न्यायालय ने 1984 के अधिनियम में “आतंकवादी कृत्य” की परिभाषा की जांच की। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि इस शब्द के इरादे और उद्देश्य 1987 के अधिनियम के समान ही थे। दोनों अधिनियमों में उन कृत्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाते हैं, न कि केवल सामान्य सार्वजनिक व्यवस्था के मुद्दों पर। सरल शब्दों में कहें तो 1984 का अधिनियम सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा के लिए अधिक गंभीर खतरों से निपटना था। इसलिए, न्यायालय ने माना कि 1984 का अधिनियम केन्द्र सरकार द्वारा वैध रूप से अधिनियमित किया गया था और इसे पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता।
क्या आरोपित अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष एवं उचित है?
यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में चुनौती दिए गए विवादित अधिनियमों के कई प्रावधानों की वैधता पर निर्णय लेने के लिए तैयार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक प्रावधान पर विचार किया, जिसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उसमें ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो अन्यायपूर्ण, अनुचित और असंवैधानिक हैं और अपना निर्णय दिया। वे इस प्रकार हैं:
1987 अधिनियम की धारा 2(1)(a)
1987 के अधिनियम की धारा 2(1)(a) के तहत प्रदत्त ‘उकसाने’ की परिभाषा के संबंध में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इस परिभाषा को इस आधार पर चुनौती दी कि यह अस्पष्ट है तथा इसमें स्पष्टता का अभाव है। उन्होंने तर्क दिया कि 1987 के अधिनियम के तहत अपराध की परिभाषा अनिश्चित और अस्पष्ट है, क्योंकि इसमें दोषी मन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, परिभाषा में ऐसी त्रुटि को दूर करने के लिए, याचिकाकर्ता ने न्यायालय द्वारा इस परिभाषा में मेन्स रीआ को शामिल करने या उसकी व्याख्या करने का प्रस्ताव रखा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक न्यायशास्त्र में अपनाए जाने वाले इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष मन से अपराध करता है तो उसे अपराध नहीं कहा जाता। अपराध करने के लिए इरादे और कार्रवाई दोनों का होना आवश्यक है। ये दोनों ही अपराध के आवश्यक घटक हैं। कोई भी कार्य अकेले अपराध नहीं माना जाता है यदि उसके साथ दोषी मन (मेन्स रीआ) न जुड़ा हो। आपराधिक कानून का यह सामान्य सिद्धांत लैटिन कहावत “एक्टस नॉन फैसिट रीम, निसी मेंस सिट रीया” (जब तक दोषी मन न हो, तब तक कोई कार्य किसी को दोषी नहीं बनाता) में सटीक रूप से समाहित है। हालाँकि, इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए न्यायालय ने इस सामान्य नियम के कुछ अपवादों को भी मान्यता दी। यह अपवाद विधायिका को कुछ परिस्थितियों में विशिष्ट कार्यों को होने से रोकने के लिए मेन्स रिया की आवश्यकता को छोड़ने की अनुमति देता है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसा अपवाद तभी लागू होगा जब उसे कानून द्वारा स्पष्टतः या परोक्ष रूप से अपवर्जित किया गया हो, और यदि उसे अपवर्जित नहीं किया गया हो, तो कानून की व्याख्या करते समय मेन्स रिया को एक आवश्यक तत्व माना जाना चाहिए। मेन्स रीआ से संबंधित सिद्धांत का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय वर्तमान मुद्दे पर विचार करने के लिए आया और कहा कि जब किसी क़ानून को चुनौती दी जाती है तो मुख्य प्रश्न “मेन्स रीआ” शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह कि क्या यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि संसद ने दोषी मन की आवश्यकता वाले सामान्य नियम से विचलित होने का इरादा किया था, विशेष रूप से ‘उकसाने’ की परिभाषा से जुड़े मामलों में।
निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा राज्य बनाम अब्दुल अजीज (1961) मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया। इस मामले में, न्यायालय ने आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 में निहित मनःस्थिति की अनुपस्थिति पर चर्चा की थी, तथा माना था कि इस धारा के तहत उल्लंघन के लिए उकसाना उल्लंघन के समान ही है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि मेन्स रिया की आवश्यकता को मुख्य या मौलिक अपराध से बाहर रखा जाता है, तो इसे उस अपराध के दुष्प्रेरण से भी बाहर रखा जाता है।
इसके बाद न्यायालय ने यह आकलन करना शुरू किया कि क्या विधानमंडल 1987 के अधिनियम के मूल अपराधों में ‘मनुष्य की मंशा’ की उपस्थिति को बाहर करने का इरादा रखता है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि 1987 के अधिनियम के कड़े प्रावधानों के बावजूद क्या इन अपराधों की परिभाषा में ‘मनुष्य की मंशा’ को शामिल करने से यह कानून अप्रभावी हो जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 1987 के अधिनियम के कई प्रावधानों का विश्लेषण किया। न्यायालय ने कहा कि 1987 के अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के अनुसार, ‘आतंकवादी’ की परिभाषा में स्पष्ट रूप से आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति की मंशा को शामिल किया गया है। इसी प्रकार, धारा 4(2)(i) और (ii) में प्रावधान है कि विघटनकारी गतिविधियों में लगे व्यक्ति में ऐसे कृत्य करने का इरादा होना चाहिए। अदालत ने पाया कि इस संबंध में 1985 और 1987 दोनों अधिनियमों की धारा 3 और 4 के प्रावधान समान हैं। इन धाराओं के विश्लेषण के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि टाडा अधिनियम के तहत मुख्य अपराधों के लिए स्पष्ट रूप से अपराधी की ओर से दुर्भावना की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, चाहे इसमें आतंकवाद या विघटनकारी गतिविधियां शामिल हों। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि चूंकि 1987 अधिनियम के मूल अपराध के लिए अपराध गठित करने की मंशा का होना आवश्यक है, इसलिए ऐसे अपराध के लिए उकसाने के लिए भी उकसाने का अपराध गठित करने की उसी मंशा की आवश्यकता होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना निर्णय देते हुए इस परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा कि यह अनिश्चित और अस्पष्ट है, तथा इससे निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की संभावना बनी रहती है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून के प्रावधान सटीक और स्पष्ट होने चाहिए ताकि ऐसे प्रावधानों के मनमाने ढंग से लागू होने से रोका जा सके। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि ‘उकसाने’ की परिभाषा की व्याख्या में मेन्स रिया की आवश्यकता को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे इसे मूल अपराधों के साथ समन्वयित किया जा सके और अनपेक्षित परिणामों को रोका जा सके। इस तरह के स्पष्टीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि निर्दोष व्यक्ति अनजाने में कानूनी मामलों में न फंस जाएं।

1987 अधिनियम की धाराएं 3 और 4
याचिकाकर्ता ने 1987 अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों को तीन आधारों पर चुनौती दी थी, अर्थात्:
- इन धाराओं में उल्लिखित अपराधों को पहले से ही भारतीय दंड संहिता, 1860, शस्त्र अधिनियम, 1959 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 जैसे मौजूदा कानूनों के तहत निपटाया जाता है।
- इस बारे में कोई उचित दिशा-निर्देश नहीं हैं कि कार्यपालिका को सामान्य कानूनों और 1987 के अधिनियम के तहत कब आगे बढ़ना चाहिए।
- ये धाराएं संविधान के अनुच्छेद 14 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) (अनवर अली मामला) के मामले में स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।
अदालत ने चुनौती दिए गए आधारों का विश्लेषण करने के बाद 1987 अधिनियम की दोनों धाराओं की वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने (1) और (2) के आधार पर की गई चुनौती को खारिज कर दिया और कहा कि आतंकवाद और व्यवधान से संबंधित वर्तमान गंभीर परिदृश्य को संबोधित करने के लिए मौजूदा कानूनों की अपर्याप्तता को दूर करने के लिए सख्त प्रावधानों और विशेष प्रक्रियाओं को शामिल करना आवश्यक है, जो भारतीय संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं। न्यायालय ने उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन बनाम गुजरात राज्य (1988) (उस्मानभाई मामला) में की गई इस टिप्पणी पर जोर दिया कि आपराधिक दंड लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। अदालत ने न्यायाधीशों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य 1987 अधिनियम के तहत लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों को अनुचित रूप से फंसाया न जाए जो कानून के दायरे में नहीं आते।
आधार (3) के आधार पर की गई चुनौती के लिए, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में अनवर अली मामले में निर्धारित सिद्धांत से संबंधित थी, अदालत ने इसे निर्णय के बाद के भाग में चर्चा के लिए स्थगित कर दिया जो अपराधों के वर्ग या वर्गों के मुद्दे और कानून के समक्ष ‘समानता के परीक्षण’ से संबंधित है। हालाँकि, इस मुद्दे पर मामले को समाप्त करने के उद्देश्य से, अदालत ने माना कि 1987 अधिनियम के तहत परीक्षणों के लिए अलग न्यायिक तंत्र के संबंध में प्रावधान भेदभाव नहीं है और इस प्रकार 1987 अधिनियम की धारा (3) और (4) में निहित प्रावधानों को बरकरार रखा गया।
1947 अधिनियम की धारा 8
संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का आकलन करके, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 1987 अधिनियम की धारा 8 (1) और (2) के तहत नामित अदालत को दी गई विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग सख्त शर्तों के तहत किया जाना चाहिए। शर्तों में लिखित रूप में जब्ती के आदेश को कम करना, यह सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि जब्त की गई संपत्ति 1987 अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की है, और आदेश में जब्त की जाने वाली संपत्ति का उल्लेख होना चाहिए। ये शर्तें यह सुनिश्चित करती हैं कि जब्ती से संबंधित आदेश उचित तर्क का हवाला देकर दिया गया है, हालांकि धारा में स्पष्ट रूप से कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि जब्ती का आदेश देने की आवश्यकता वाले प्रावधान में अदालत द्वारा निर्णय या निर्देश शामिल है, जिसके लिए उसके निर्णय का औचित्य आवश्यक है। न्यायालय ने 1987 अधिनियम की धारा 19 का भी उल्लेख किया, जिसके तहत 1987 अधिनियम के तहत पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति तथ्यात्मक और कानूनी दोनों आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जब्ती के आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इस प्रकार, न्यायालय द्वारा उपरोक्त की गई टिप्पणी के आधार पर, यह माना गया कि धारा 8 की वैधता को चुनौती देने वाली दलीलें निराधार थीं।
1987 अधिनियम की धारा 9
याचिकाकर्ता द्वारा 1987 अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता को दो आधारों पर चुनौती दी गई थी। चुनौती का पहला आधार यह था कि यह धारा सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 65 और संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और 235 का उल्लंघन है। ये अनुच्छेद राज्य द्वारा जिला न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र और नियुक्ति से संबंधित हैं। दूसरा आधार यह था कि धारा 9 की उपधारा 9(7) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अदालत ने उन आधारों की जांच की जिन पर धारा 9 के प्रावधान को चुनौती दी गई थी और प्रत्येक आधार की वैधता पर निर्णय दिया।
प्रथम आधार पर निर्णय करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका है कि 1987 का अधिनियम सूची I की प्रविष्टि 1 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया था, जो संसद को ऐसे कानून बनाने की विधायी क्षमता प्रदान करता है, इसलिए, अधिनियम की धारा 9 द्वारा अधिकृत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नामित न्यायालयों का गठन, सूची II की प्रविष्टि 65 का उल्लंघन नहीं करता है। प्रविष्टि 65 राज्य विधानमंडलों को न्यायालय गठित करने का अधिकार देती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि संघ द्वारा स्थापित निर्दिष्ट न्यायालय का क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट क्षेत्रों में किए गए अपराधों पर आधारित है। ऐसा क्षेत्राधिकार इस तथ्य से अप्रभावित है कि निर्दिष्ट न्यायालय की स्थापना के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि अधिकार क्षेत्र के प्रश्नों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देने से संबंधित धारा 9 के प्रावधान किसी भी तरह से इस धारा की संवैधानिकता को खत्म नहीं करते हैं। परिणामस्वरूप, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 9 सूची II की प्रविष्टि 65 और संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और 235 का उल्लंघन है।
जहां तक दूसरे आधार का सवाल है, जिसमें धारा 9(7) की वैधता को चुनौती दी गई थी, अदालत ने माना कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। इसने माना कि खंड (7) के प्रावधान जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी नामित न्यायालय में न्यायाधीश की सेवा जारी रखने की अनुमति देते हैं, वे न्यायिक स्वतंत्रता और परीक्षणों में निष्पक्षता को कमजोर नहीं करते हैं। न्यायालय ने विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 बनाम अज्ञात (1978) मामले में अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क को भी खारिज कर दिया। इस मामले में, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए विधेयक या उसके किसी प्रावधान की संवैधानिकता के प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया। इस धारा के अंतर्गत, किसी विशेष न्यायालय की अध्यक्षता किसी उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो पहले किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद संभाल चुका हो, तथा जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो। इस प्रावधान पर विचार करने के बाद न्यायालय ने माना कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही किसी विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति देती है। वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 के संबंध में की गई टिप्पणी को स्वीकार किया, तथापि, न्यायालय ने इसे वर्तमान स्थिति से अलग बताया। न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश का पद संभालना, विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति से भिन्न है। अदालत ने निर्देश दिया कि नामित न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय प्राधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि शुरू से ही सेवा की पर्याप्त अवधि हो, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद सेवा जारी रखने की न्यूनतम संभावना हो। इसलिए, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित आधारों पर धारा 9(7) असंवैधानिक नहीं थी।
1987 अधिनियम की धारा 20 (3)
इन धाराओं के तहत, स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अलावा कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शामिल करने पर सवाल उठाया, जिन्हें 1973 संहिता की धारा 167(1) के तहत स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति या बयान दर्ज करने के लिए अधिकृत करने से अनैच्छिक स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा और इस प्रकार यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत असंवैधानिक होगा। इसके अतिरिक्त, इस समावेशन से संविधान के अनुच्छेद 50 में उल्लिखित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट जैसे गैर-न्यायिक प्राधिकारियों में न्यायिक निष्ठा और स्वतंत्रता का अभाव है, इसलिए उन्हें न्यायिक कार्य सौंपने से अनुच्छेद 50 के शासन सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इन तर्कों का खंडन करने के लिए विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। इसकी शुरुआत 1973 संहिता की धारा 6 और 20 पर प्रकाश डालने से हुई, जिसके तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हर राज्य में आपराधिक न्यायालयों की एक श्रेणी में माना जाता था। इस ढांचे का उद्देश्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों (उच्च न्यायालय के अधीन) और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (राज्य सरकार के अधीन) के बीच मजिस्ट्रेटीय कार्यों का आवंटन करके अखिल भारतीय स्तर पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की एक सरल योजना को प्राप्त करना था। अदालत ने कहा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट मुख्य रूप से प्रशासनिक और पुलिस संबंधी कार्यों के साथ-साथ कुछ न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों को संभालने के लिए अधिकृत हैं। अन्य आपराधिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की तरह, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश भी पुनरीक्षण योग्य होते हैं क्योंकि वे न्यायिक कार्यवाही में पारित किए जाते हैं। न्यायालय ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों के न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों को मान्यता दी, जो उन्हें 1973 संहिता के तहत सौंपे गए थे और इस प्रकार, यह टिप्पणी की गई कि इन मजिस्ट्रेटों को आपराधिक मामलों के निर्णय तंत्र से बाहर नहीं माना जा सकता।
अदालत ने 1973 संहिता के विभिन्न प्रावधानों जैसे धारा 107, 108, धारा 167 की उपधारा 2-A आदि का उल्लेख किया, जिसमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट को न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अभियुक्त को हिरासत में लेना और जमानत पर रिहा करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 1973 संहिता के अध्याय VIII (शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा) में यह भी प्रावधान है कि वे शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण के लिए सुरक्षा से संबंधित कार्यवाही में भी शामिल हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किया गया था और इसलिए, यह आपराधिक न्यायशास्त्र के स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप है।
इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायिक अधिकारी हैं या नहीं। न्यायालय ने ‘न्यायिक अधिकारी’ शब्द का विश्लेषण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारी माना जा सकता है। अदालत ने श्री कुमार पद्म प्रसाद बनाम भारत संघ (1992) के मामले का उल्लेख किया, जिसमें ‘न्यायिक अधिकारी’ शब्द को परिभाषित किया गया था। इस मामले में अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस शब्द में न्याय प्रशासन से जुड़े पदों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अदालत ने आगे कहा कि 1973 संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करते हुए, सरकारी पदों पर आसीन या रह चुके व्यक्ति विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए न्यायिक कार्य कर सकते हैं।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) के मामले में दिए गए निष्कर्षों का अवलोकन किया और माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्तियों में विभेदीकरण किया गया है, ताकि एक को दूसरे के कार्यों को संभालने से रोका जा सके। हालांकि, कार्यपालिका उन मामलों पर कानून बना सकती है, यदि उसे विधायिका द्वारा कार्य सौंपे गए हों और कुछ परिस्थितियों में न्यायिक कार्य भी कर सकती है, बशर्ते ऐसी शक्ति का प्रयोग संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाए।
ऊपर चर्चा किए गए विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब कार्यकारी मजिस्ट्रेट को न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है, तो उन्हें न्यायिक अधिकारी माना जाता है। इस प्रकार, यह माना गया कि 1987 अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) संविधान के अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन नहीं करती है। हालाँकि, न्यायालय ने कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की न्यायिक अखंडता और स्वतंत्रता की संभावित कमी के बारे में विद्वान वकील द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया। इस प्रकार, इस चिंता को दूर करने के लिए, अदालत ने निर्देश दिया कि प्रयास किए जाने चाहिए कि स्वीकारोक्ति या बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए, यदि वे उपस्थित हों। कार्यकारी या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही स्वीकारोक्ति या बयान दर्ज कर सकते हैं, तथा ऐसा तब भी कर सकते हैं जब उनके शामिल होने के लिए वैध कारण मौजूद हों।
1987 अधिनियम की धारा 22
श्री जेठमलानी द्वारा प्रस्तुत तर्क, जैसा कि उनके लिखित प्रस्तुतिकरण में रेखांकित किया गया है, यह है कि 1987 के अधिनियम की धारा 22 समझ से परे और अव्यावहारिक थी। उन्होंने तर्क दिया कि केवल तस्वीर के आधार पर किसी व्यक्ति की सटीक पहचान करना असंभव है, विशेषकर ऐसे युग में जब ट्रिक फोटोग्राफी प्रचलित हो।
इस तर्क पर विचार करने के बाद न्यायालय इस बात से सहमत हुआ कि पहचान के लिए केवल फोटोग्राफिक साक्ष्य पर निर्भर रहना घोर अन्याय का कारण बन सकता है, विशेषकर जब इसकी तुलना पहचान परेड के माध्यम से प्राप्त साक्ष्य से की जाए। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने 1987 अधिनियम की धारा 22 को रद्द करने का निर्णय लिया।
क्या पुलिस के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है तथा संवैधानिक है?
1987 के अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, पुलिस अधीक्षक से निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी द्वारा संस्वीकृति दर्ज करने से न केवल आरोपी को दुर्व्यवहार और मानवाधिकार हनन से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आत्म-दोषी ठहराए जाने का जोखिम भी कम होगा। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे इकबालिया बयानों में 1973 संहिता की धारा 164 और साक्ष्य अधिनियम के तहत निहित आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए। 1987 अधिनियम की धारा 15 को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) नियम, 1987 के नियम 15 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसके तहत स्वीकारोक्ति दर्ज करने वाली पुलिस को कुछ कानूनी औपचारिकताओं और शर्तों का पालन करना होता है। इस प्रकार, इस तर्क के आधार पर, धारा 15 को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने पन्नालाल बिंजराज बनाम भारत संघ (1957) के मामले में की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी कानूनी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना मात्र उसे असंवैधानिक मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
1987 के अधिनियम की धारा 15 को भी इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसलिए, वर्तमान मामले में न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 के संबंध में धारा 15 की वैधता पर निर्णय लेने के लिए ‘अपराधियों’ और ‘अपराधों’ के वर्गीकरण की जांच करना आवश्यक समझा। अदालत ने कहा कि विधायी वर्गीकरण का सिद्धांत विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत व्यक्तियों के उपचार में विभेदीकरण की अनुमति देता है। यह सिद्धांत यह मानता है कि कानून विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अंतर कर सकता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि भिन्न परिस्थितियों वाले एक समूह पर जो लागू होता है, वह आवश्यक रूप से दूसरे पर भी लागू नहीं होता। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार का असमान व्यवहार न हो, क्योंकि प्रत्येक समूह को उनकी विशिष्ट स्थितियों और परिस्थितियों के लिए बनाए गए अलग-अलग कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है। हालाँकि, ऐसा वर्गीकरण तभी वैध माना जाएगा जब ऐसे विभेदकारी व्यवहार के लिए उचित औचित्य हो। वर्गीकरण मनमाना नहीं बल्कि वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत होना चाहिए। उपचार में इस तरह के अंतर को उस उद्देश्य के साथ संबंध को उचित ठहराना चाहिए जिसके लिए वर्गीकरण किया गया है।
इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 1987 के अधिनियम के तहत किए गए वर्गीकरण की जांच की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वर्गीकरण और भेद संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में वैध और उचित है। 1987 के अधिनियम ने आतंकवादियों और विध्वंसकारी तत्वों को नियमित कानूनों के अंतर्गत सामान्य अपराधियों से अलग वर्गीकृत किया तथा अपराधों को सामान्य अपराधों से अलग गंभीर अपराधों के रूप में परिभाषित किया। तर्कसंगतता निर्धारित करने के लिए, वर्गीकरण के पीछे के उद्देश्य पर प्रस्तावना के साथ-साथ 1987 के अधिनियम के ‘उद्देश्यों और कारणों के कथन’ से भी विचार किया जाना चाहिए। इस कानून को लागू करने में केंद्र सरकार की योग्यता के मुद्दे पर निर्णय करते हुए यह न्यायालय पहले ही यह मान चुका है कि जिन कारणों और उद्देश्यों के लिए 1987 का अधिनियम लागू किया गया था, वे वैध हैं और इसलिए, इसके तहत किया गया वर्गीकरण भी वैध है।
न्यायालय ने इस मुद्दे के संबंध में उठाए गए तर्कों का निपटारा करते हुए कहा कि अनवर अली मामले में लिया गया निर्णय, जिसके निष्कर्षों पर याचिकाकर्ताओं ने भारी भरोसा किया था, वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता। अदालत ने कहा कि विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 की धारा 5 के संबंध में अनवर अली मामले में अदालत का निर्णय यह था कि इस अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में विचारण हेतु अपराधों के वर्गीकरण के लिए कानून में कोई आधार नहीं है और इसके अतिरिक्त किसी भी मामले को विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करना पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया था। इस मामले के निष्कर्षों की जांच करने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस निर्णय का उपयोग 1987 के अधिनियम की धारा 15 को अमान्य करने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 1987 के अधिनियम के तहत निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने वाले अपराधों और अपराधियों का वर्गीकरण केन्द्र सरकार के विवेक पर नहीं छोड़ा गया था और 1987 के अधिनियम और 1984 के अधिनियम दोनों के तहत आतंकवादियों और विघटनकारी के रूप में अपराधियों का स्पष्ट और वैध वर्गीकरण था।
क्या 1973 संहिता की धारा 438 को अप्रभावी बनाने वाला प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है और क्या विधानमंडल के पास इसकी प्रयोज्यता को हटाने की क्षमता है?
1987 अधिनियम की धारा 20(7) के संबंध में इस विशेष मुद्दे पर अपना निर्णय समाप्त करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बिमल कौर खालसा बनाम भारत संघ और अन्य (1987) (बिमल कौर मामला) के मामले में किए गए निष्कर्षों का अवलोकन किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1987 अधिनियम की धारा 20(7) की वैधता को बरकरार रखा था। इसने तर्क दिया कि आतंकवादी कृत्यों के अभियुक्त व्यक्ति एक अलग वर्ग का गठन करते हैं और इसका तात्पर्य यह है कि अग्रिम जमानत से इनकार करने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गिरफ्तार आतंकवादियों से प्रभावी पूछताछ की गारंटी मिलती है, ताकि वे महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा कर सकें, जो समाज में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 1973 संहिता से संबंधित कानून बनाने की विधायी शक्ति संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों में निहित है। इसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि अग्रिम जमानत प्रावधान पुरानी संहिता का हिस्सा नहीं थे, जिन्हें बाद में विधि आयोग और संयुक्त समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप 1973 की संहिता में शामिल किया गया था। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित अग्रिम जमानत से संबंधित विभिन्न राज्यवार संशोधनों पर विचार-विमर्श किया तथा इस संबंध में विधायी लचीलेपन का सुझाव दिया। न्यायालय ने अग्रिम जमानत लागू करने के विधि आयोग के तर्क पर गौर किया तथा इस बात पर बल दिया कि यह जमानत उन मामलों में न्यायोचित नहीं है जहां यह माना जाता है कि आरोपी व्यक्ति फरार हो सकता है या अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि धारा 438 एक नया प्रावधान है जो एक नया अधिकार सृजित करता है, इसलिए इसे हटाने से धारा 21 का उल्लंघन नहीं होता है, जैसा कि गुरबख्श सिंह सिब्बिया आदि बनाम पंजाब राज्य (1980) में कहा गया था। इस प्रकार, धारा 20 की उपधारा (7) की वैधता की चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती।
न्यायालय ने इस मुद्दे को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1976 की धारा 9 की संवैधानिक वैधता को दी गई चुनौती के संबंध में भी अपना निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि चूंकि इस धारा की वैधता को 1987 के अधिनियम की धारा 20(7) के समान ही चुनौती दी गई थी, इसलिए वही टिप्पणियां लागू होंगी और इसलिए ऐसी टिप्पणियों के आधार पर, यह तर्क कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है, खारिज कर दिया गया।

क्या संहिता की धारा 437(3) में निहित सीमाओं के अतिरिक्त जमानत देने पर गंभीर सीमाएं लगाना उचित एवं न्यायोचित है?
अदालत ने 1987 के अधिनियम की धारा 20 (8) पर विचार किया, जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि आवश्यक शर्तें पूरी न हो जाएं। इसमें उल्लेख किया गया है कि इस प्रतिबंध में दो शर्तों के तहत छूट दी गई है: सबसे पहले, सरकारी अभियोजक को जमानत आवेदन पर आपत्ति करने का अवसर दिया जाना चाहिए और दूसरी बात, अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह स्वीकार करने के लिए संभावित आधार हैं कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और अभियुक्त द्वारा जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त, परिच्छेद (9) में यह स्पष्ट किया गया कि जमानत देने पर ये प्रतिबंध दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य कानून में निर्धारित प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं।
इसके बाद, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, 437, 438 और 439 के प्रासंगिक प्रावधानों का वर्णन किया, जो विशेष रूप से जमानत से संबंधित हैं। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि धारा 437 जमानत देने पर कुछ शर्तें लगाती है, जो कि न्याय के हित में आवश्यक समझी जाने वाली शर्तें लगाने के लिए धारा 437(3) के तहत न्यायालय को दिए गए विवेक के अधीन है। अदालत ने “उस्मानभाई मामले” में सहमति व्यक्त की जिसमें कहा गया था कि भले ही जमानत 1987 अधिनियम की धारा 20(8) में प्रदान की गई किसी भी सीमा के अधीन है, यह आवश्यक रूप से धारा 439 से बंधा नहीं है, जो जमानत देने के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को दी गई विशेष शक्तियों से संबंधित है। इसके बजाय, नामित न्यायालय की शक्ति का स्रोत धारा 437 है, साथ ही 1987 अधिनियम की धारा 20(8) में निर्धारित अन्य प्रतिबंध भी हैं।
अदालत ने धारा 20(8)(b) के तहत निर्धारित मानदंडों की जांच जारी रखी और निष्कर्ष निकाला कि वे संहिता की धारा 437(1) और (3) और अन्य अधिनियमों में इसी तरह के प्रावधानों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं। इस प्रकार, इस तर्क को अस्वीकार कर दिया गया कि ये शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन थीं। इसके बाद, न्यायालय ने बिमल कौर मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जिसमें लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के महत्वपूर्ण तंत्र को दोहराते हुए और पीड़ितों एवं उनके परिवारों के साथ-साथ समुदाय और नागरिकों के हितों पर विचार करते हुए धारा 20(8)(b) के हिस्से को अधिकारहीन करार दिया गया था।
न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, तथापि इन शक्तियों का परिमाण स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप तर्कसंगत और सतर्क उपयोग की मांग करता है। 1987 के अधिनियम में व्यक्त विधानमंडल की मंशा और उद्देश्य ने जमानत और अपील पर विशेष उपायों की आवश्यकता को प्रदर्शित किया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि 1987 के अधिनियम के विशेष प्रावधान, जैसे धारा 25 और धारा 20(7) में गैर-बाधा खंड, इस बात का प्रमाण हैं कि जमानत से संबंधित सभी मुद्दों को पूरी तरह से इन प्रावधानों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, यदि कोई पक्ष जमानत आदेश से खुश नहीं है तो अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना उचित उपाय है।
न्यायालय का मत था कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने से 1987 के अधिनियम की योजना और उद्देश्य विफल हो जाएंगे तथा संसद की मंशा भी विफल हो जाएगी। फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त है, तथापि उक्त शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम अब्दुल हामिद हाजी मोहम्मद (1994) मामले में की गई टिप्पणी को दोहराया कि न्यायाधीशों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका क्षेत्राधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी से और केवल असाधारण मामलों में ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि न्यायिक अनुशासन और न्यायालय पदानुक्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। इसने उच्च न्यायालयों को सलाह दी कि वे 1987 के अधिनियम जैसे किसी विशेष अधिनियम के तहत किसी व्यक्तिगत आरोपी की जमानत के आवेदन पर विचार न करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें सही करने की न्यायिक शक्ति प्राप्त है।
असहमतिपूर्ण निर्णय
इस मामले में दो न्यायाधीशों ने असहमतिपूर्ण राय दी। यद्यपि न्यायमूर्ति के. रामास्वामी और न्यायमूर्ति सहाय ने अधिकांश मुद्दों पर बहुमत से सहमति व्यक्त की, लेकिन उन्होंने बहुमत वाले न्यायाधीशों द्वारा दिए गए दो निर्णयों के संबंध में असहमति व्यक्त की थी। ये थे 1987 अधिनियम की धारा 9(7) और धारा 15 की संवैधानिक वैधता। इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति रामास्वामी ने एक अन्य निर्णय पर भी असहमति व्यक्त की, जो टाडा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत जमानत देने संबंधी उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।
1987 अधिनियम की धारा 9(7)
न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि धारा 9 की उप-धारा (7), जिसमें यह प्रावधान है कि नामित न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु (सेवानिवृत्ति की आयु) तक पहुंचने के बाद भी सेवा में बने रहेंगे, न्यायाधीश की सेवा को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु की परवाह किए बिना, केंद्र या राज्य सरकार के विवेक पर रखने की विधायी मंशा को इंगित करता है। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अभियुक्तों में इसके प्रति पैदा होने वाले विश्वास पर इन प्रावधानों के प्रभाव के बारे में चिंता जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि इस धारा की संवैधानिक वैधता का निर्धारण उपर्युक्त निहितार्थों के अनुरूप किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति रामास्वामी ने बहुमत के आधार पर निर्दिष्ट न्यायालय के गठन की वैधता को स्वीकार किया, तथापि, दो विशिष्ट पहलुओं के संबंध में चिंता जताई गई जिन्हें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विपरीत माना गया।
- उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण के बिना निर्दिष्ट न्यायालयों में सत्र न्यायाधीशों या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त न्यायिक अंतरनिर्भरता के सिद्धांत का उल्लंघन है। नियंत्रण की ऐसी कमी से न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई, जिससे न्यायिक स्थिति कार्यपालिका के प्रभाव के लिए खुली हो गई।
- उन्होंने उस प्रावधान की आलोचना की, जो नामित न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद भी सेवा जारी रखने की अनुमति देता है। इस प्रथा के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां एक न्यायाधीश को न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा जारी रखने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की निष्पक्षता और अखंडता का घोर उल्लंघन होता है।
अपने द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने बहुमत के निर्णय से असहमति जताते हुए कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति “आनंद सिद्धांत” के माध्यम से की जाती है, जिसका तात्पर्य योग्यता और स्वतंत्रता के आधार पर नियुक्त किए जाने के बजाय सरकार की इच्छा पर काम करने वाले न्यायाधीशों से है, जो न्याय की बुनियाद और उस निष्पक्षता को कमजोर करता है जिसके साथ न्यायपालिका से काम करने की उम्मीद की जाती है। इसलिए, धारा 9(7) का प्रावधान इस आधार पर असंवैधानिक है कि वे स्वतंत्र न्यायपालिका के मूल सिद्धांत के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
1987 अधिनियम की धारा 15
न्यायमूर्ति रामास्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुझाव दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत उल्लिखित प्रक्रिया में आपराधिक कार्यवाही में सच्चाई का पता लगाने का तरीका भी शामिल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जांच की प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने अपना असहमतिपूर्ण निर्णय सुनाते हुए 1973 संहिता की धारा 36 का उल्लेख किया। यह धारा स्थानीय क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों या पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती है। उन्होंने 1973 संहिता की धारा 2(h) का भी उल्लेख किया जो जांच प्रक्रिया को परिभाषित करती है और इसमें प्राधिकृत मजिस्ट्रेटों को छोड़कर पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए साक्ष्य संग्रह की सभी कार्यवाहियां शामिल हैं। इन प्रावधानों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिस हिरासत में व्यक्तियों से संस्वीकृति दर्ज करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान ईमानदारी और तटस्थता बरतता है।
उन्होंने आगे सवाल उठाया कि क्या 1987 के अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत गैर बाधा खंड (नॉन-ऑब्स्टेंटे क्लॉज) (एक कानूनी प्रावधान जो विरोधाभासी प्रावधानों के बावजूद किसी कार्य को प्रभावी होने की अनुमति देता है) को शामिल करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित कानूनी सिद्धांतों को कम करने वाली प्रक्रियाओं की गारंटी या वैधता मिलती है।

अपने निर्णय के समर्थन में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 के मामले का उल्लेख किया, जिसमें निर्धारित प्रक्रिया को अभियुक्त के लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण माना गया था और इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन था। इस मामले का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास और भरोसा हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि पुलिस अधिकारियों को न्यायिक कार्य सौंपने से जनता का विश्वास और कानून के शासन की प्रभावशीलता कमजोर होती है। इसलिए, पुलिस अधीक्षक के बराबर या उससे उच्च रैंक का एक पुलिस अधिकारी, जो कानून और व्यवस्था के समुचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराध के दमन के लिए लगन से प्रयास करेगा और ऐसी जिम्मेदारी को पूरा करने में आपराधिक गतिविधियों को रोकने और गलत काम करने वालों के दिलों में डर पैदा करने के लिए सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करेगा।
यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहां कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए अपराधों के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय होना महत्वपूर्ण है, वहीं न्याय की पूर्ण डिलीवरी के लिए संदिग्धों के मन से किसी भी संदेह को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। इस कारण से, पुलिस अधिकारियों द्वारा इकबालिया बयान दर्ज करना कानून के शासन को कमजोर करता है और संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत उल्लिखित संवैधानिक सिद्धांतों का खंडन करता है। इस प्रकार धारा 15 को अन्यायपूर्ण, अनुचित तथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला माना गया।
टाडा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार
न्यायमूर्ति रामास्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उत्थान के लिए रिट और निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अप्रतिबंधित अधिकार को मान्यता दी और इस प्रकार कहा कि विधायिका को किसी भी तरह से उच्च न्यायालय के इस अधिकार क्षेत्र को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि 1987 का अधिनियम विशेष और गंभीर प्रकार के अपराधों से संबंधित है, इसलिए निर्दिष्ट न्यायालय में इन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि धारा 19, जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देती है, उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के मामलों से निपटने के अधिकार से वंचित करती है। इसमें उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह से बाहर रखा गया, जिसके कारण कानून की प्रभावकारिता में अनिश्चितता और अविश्वास पैदा हो गया।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) का आज महत्व
बहुमत से लिए गए इस निर्णय की विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा कड़ी आलोचना की गई। 1987 के अधिनियम की धारा 15 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत में जनता के बीच बहस का केन्द्र था। 3:2 के बहुमत से इस धारा को बरकरार रखने को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का सीधा उल्लंघन है। हालांकि, न्यायमूर्ति रामास्वामी और न्यायमूर्ति सहाय द्वारा दिए गए असहमतिपूर्ण निर्णयों की सराहना की गई और उन्हें निष्पक्ष सुनवाई, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, तथा स्वतंत्रता की अधिक सुरक्षा के लिए कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण और संतुलन के प्रयोग के संबंध में चर्चा का आधार माना गया।
असहमति जताने वाले न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियां अब व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा के बीच संघर्ष सहित मामले पर निर्णय लेने का आधार बन गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी बनाम नवजोत संधू (2005) मामले में, जिसे आमतौर पर संसद हमला मामले के रूप में जाना जाता है, फैसला सुनाया कि पुलिस उपायुक्त द्वारा दर्ज अभियुक्त से प्राप्त इकबालिया बयान अवैध है। न्यायालय ने माना कि पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई संस्वीकृति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय और स्वीकार्य नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग तथा आपराधिक न्याय प्रणाली में दबावपूर्वक या अविश्वसनीय बयानों के विरुद्ध संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में चिंता को उजागर करता है।
संक्षेप में, रामास्वामी द्वारा व्यक्त असहमति हमें कार्यपालिका के अतिक्रमण के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रियाओं के संरक्षण को प्राथमिकता देने का आग्रह करती है। संविधान का अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता के अधिकार को मौलिक मानता है तथा इससे किसी भी प्रकार का वंचित करना अपवाद माना जाता है। 1978 में 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 359 में सरकार द्वारा पालन की जाने वाली अपेक्षित प्रक्रिया को शामिल किया जाना, आपातकालीन प्रावधानों के दौरान भी, इसके अत्यंत महत्व को रेखांकित करता है, जो मनमाने उल्लंघनों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण जांच के रूप में कार्य करता है। आपराधिक न्याय प्रणाली के ढांचे के भीतर, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों, अभियुक्तों और व्यापक जनता की साझा जिम्मेदारी होती है, जिन सभी को न्याय को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क निगरानी रखने का काम सौंपा जाता है।
करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) मामले के बाद परिवर्तन
मामले में लिए गए निर्णय के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए और 1987 के अधिनियम को वापस लेने की मांग उठी, और अंततः 1995 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। फिर भी, निरसन में एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि टाडा के तहत दर्ज मामले जारी रह सकते हैं। परिणामस्वरूप, अनेक टाडा मामले अभी भी लंबित हैं, तथा उन पर जांच और कानूनी कार्यवाही जारी है।
मार्च 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 (पोटा अधिनियम) लागू हुआ, जिसमें 1987 अधिनियम के समान प्रावधान थे। पोटा अधिनियम के प्रावधानों को पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2004) मामले में चुनौती दी गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी वैधता बरकरार रखी। वर्ष 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई तो उसने पोटा कानून को निरस्त कर दिया।
यद्यपि इन अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन यह केवल प्रतीकात्मक है, क्योंकि कई कड़े प्रावधानों को 2004 और 2008 में संशोधनों के माध्यम से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए अधिनियम) में एकीकृत कर दिया गया था। 2019 में हाल ही में किए गए संशोधनों ने केंद्र सरकार की शक्तियों का और विस्तार किया, जिससे उसे व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने में सक्षम बनाया गया। इन विधायी कदमों ने एक जटिल स्थिति पैदा कर दी है, जहां अब एक ही अपराध को अलग-अलग तरीके से निपटाया जा सकता है, तथा जांच और सुनवाई के लिए अलग-अलग नियम होंगे।

निष्कर्ष
यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रस्तुत करता है। यद्यपि बहुमत ने विवादित अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन न्यायमूर्ति रामास्वामी और न्यायमूर्ति सहाय द्वारा 1987 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को निरस्त करते हुए दिए गए असहमतिपूर्ण निर्णयों ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि यद्यपि आतंकवाद राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इसका मुकाबला करने के लिए कड़े कानूनों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है, यह हर समय सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग न हो और अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
सार और तत्व के सिद्धांत का क्या अर्थ है?
सार और तत्व का सिद्धांत तब अपनी भूमिका निभाता है जब इस बात पर संदेह होता है कि किसी विशेष विधायिका (संघ या राज्य) के पास कानून बनाने का अधिकार है या नहीं। ऐसा संदेह तब होता है जब एक सूची में शामिल विषय-वस्तु से संबंधित कानून किसी अन्य सूची में शामिल विषय-वस्तु को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में कानून का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य, उसका “वास्तविक उद्देश्य” अर्थात् कानून का सार और सार जानना महत्वपूर्ण हो जाता है।
1987 अधिनियम की सबसे विवादास्पद धारा कौन सी थी?
1987 के अधिनियम की सबसे विवादास्पद धारा धारा 15 थी। इस धारा के अनुसार, पुलिस अधीक्षक से नीचे के स्तर का पुलिस अधिकारी अभियुक्तों की संस्वीकृति और बयान दर्ज करने के लिए प्राधिकृत था, तथा ऐसी संस्वीकृति और बयान, उन्हें देने वाले अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य माने जाते थे।
इस मामले में असहमतिपूर्ण निर्णय किसने दिया?
न्यायमूर्ति रामास्वामी और न्यायमूर्ति सहाय ने 1987 अधिनियम के दो मुद्दों, यानी 1987 अधिनियम की धारा 9(7) और धारा 15 के संबंध में असहमतिपूर्ण निर्णय दिया। इनके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने 1987 के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जमानत देने से उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने के मुद्दे पर भी असहमतिपूर्ण निर्णय दिया।
संदर्भ







