यह लेख Subhangee Biswas द्वारा लिखा गया है। लेख में शिक्षा से संबंधित प्रविष्टियों की पृष्ठभूमि में गुजरात विश्वविद्यालय बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर के फैसले और भारत के संविधान के तहत “सामंजस्यपूर्ण व्याख्या” के सिद्धांत के अनुप्रयोग पर चर्चा की गई है। लेख में मामले के तथ्यों के साथ-साथ दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का भी उल्लेख किया गया है। कानूनी उदाहरणों से जुड़ी कानूनी अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए और उनकी व्याख्या करते हुए, लेख निर्णय और मामले के समग्र विश्लेषण के साथ समाप्त होता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर एवं अन्य (1963) का मामला इस प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या कोई विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रदान करने और परीक्षा आयोजित करने के माध्यम के रूप में किसी विशेष भाषा को लागू कर सकता है। इस मामले में गुजरात विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए गुजराती और हिंदी को शिक्षण माध्यम के रूप में लागू करना चाहता था। जब यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, तो उसने भारत के संविधान के प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की, तथा कहा कि शिक्षा के संबंध में संघ सूची के तहत संसद की शक्ति और राज्य सूची के तहत राज्य को दी गई शक्ति के बीच टकराव की स्थिति में, पूर्व की शक्ति को बाद की शक्ति पर वरीयता (प्रेफरेंस) दी जाएगी तथा राज्य की शक्ति हमेशा सीमित होगी, निरपेक्ष (एबसॉल्यूट) नहीं होगी। आइये इस मामले पर विस्तार से विचार करें और इसमें शामिल प्रावधानों पर चर्चा करें।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर और अन्य
- मामला संख्या: सिविल अपील संख्या 234 और 262, 1962
- समतुल्य उद्धरण: एआईआर 1963 एससी 703; (1963) जीएलआर 450 (एससी); 1962 आईएनएससी 263; [1963] सप्प 1 एससीआर 112
- संबंधित क़ानून और संविधि:
- अनुच्छेद 254(1)
- सातवीं अनुसूची, सूची I, प्रविष्टि 66
- सातवीं अनुसूची, सूची II, प्रविष्टि 11
- गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949
- विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा तैयार संविधि 207, 208 और 209, 1961 में संशोधित किए गए।

- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर सिन्हा, न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, न्यायमूर्ति के. सुब्बाराव, न्यायमूर्ति के.एन. वांचू, न्यायमूर्ति एन. राजगोपाल अयंगर और न्यायमूर्ति सैयद जाफर इमाम।
- फैसले की तारीख: 21 सितंबर 1962
- अंतिम निर्णय: बहुमत वाली पीठ ने 5:1 के अनुपात में अपीलों को खारिज कर दिया और गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया। प्रत्यर्थियो के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसमें आदेश दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम के रूप में दो भाषाओं के उपयोग को अनिवार्य बना सकता है, लेकिन ऐसी शक्ति अधिनियम के संबंधित प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित है।
मामले के तथ्य
पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता के पुत्र श्रीकांत ने मार्च 1960 में बम्बई राज्य द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा अपनी मातृभाषा मराठी के माध्यम से उत्तीर्ण की। इसके बाद श्रीकांत को सेंट जेवियर्स महाविद्यालय में कला वर्ग में दाखिला मिल गया, जो गुजरात विश्वविद्यालय से संबद्ध था। जिस कक्षा में उन्होंने प्रवेश लिया, वहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी।
श्रीकांत ने अपना पहला कला पाठ्यक्रम मार्च 1961 में पूरा किया। इसके अलावा, उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से मध्यवर्ती (इंटरमीडिएट) कला परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन किया।
प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 (जिसे आगे “अधिनियम” के रूप में उल्लेख किया गया है) और 1961 में संशोधित विश्वविद्यालय के सीनेट द्वारा तैयार किए गए संविधि 207, 208 और 209 के अनुसार, विश्वविद्यालय की पूर्व सहमति के बिना, उन्हें उन कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिनमें शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है।
अपीलकर्ता, जो श्रीकांत के पिता हैं, ने इसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति से संपर्क किया तथा श्रीकांत को उक्त कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति मांगी। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने ऐसी अनुमति देने से इनकार करते हुए श्रीकांत को परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रखने की अनुमति दी, लेकिन शिक्षण के माध्यम के रूप में नहीं।
22 जून 1961 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को संबोधित करते हुए एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी किया गया। परिपत्र में कहा गया कि कुलपति ने गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 11(4)(a) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- केवल ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से पूरी की है और 1960-1961 में प्रथम वर्ष (पूर्व-विश्वविद्यालय) कला वर्ग में अंग्रेजी माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखी है, उन्हें वर्ष 1961-1962 के लिए मध्यवर्ती कला वर्ग में परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।
- महाविद्यालयो को निर्देश दिया गया कि वे उपर्युक्त विद्यार्थियों को केवल एक वर्ष, अर्थात् 1961-62 के लिए अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करें।
- प्रधानाचार्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंग्रेजी को परीक्षा माध्यम बनाने की व्यवस्था से केवल उक्त विद्यार्थियों को ही लाभ मिले।
श्रीकांत को छात्रों के इस वर्ग में शामिल होने की पात्रता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा अंग्रेजी में नहीं, बल्कि मराठी में दी थी। इस तथ्य के बावजूद, यदि प्रधानाचार्य ने फिर भी श्रीकांत को अनुमति दे दी होती, तो महाविद्यालय पर अधिनियम 1949 की धारा 38A के तहत दंड लगाया जा सकता था।
गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका
इसके बाद अपीलकर्ता ने स्वयं और अपने बेटे, जो उस समय नाबालिग था, की ओर से गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें निम्नलिखित के लिए परमादेश (मैण्डमस) रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की मांग की गई-
- गुजरात विश्वविद्यालय को गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 4(27) (शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और समुदायों के बीच विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रावधान करने की विश्वविद्यालय की शक्ति), धारा 18(1) (विश्वविद्यालय की प्रगति और विकास के संबंध में सामान्य नीति के मामलों पर विचार करने और निर्णय लेने की अदालत की शक्ति), 18(14) संशोधित अधिनियम की धारा 18(13) (गुजराती या हिंदी या दोनों को शिक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने के लिए संविधि बनाने की सीनेट की शक्ति), और धारा 38A (विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लेना; और संविधि 207, 208 और 209 की शर्तों और प्रक्रिया को शून्य और अप्रभावी घोषित करना तथा ऐसे प्रावधानों पर कार्रवाई करने या उन्हें लागू करने से बचना;
- कुलपति को निर्देश देना कि वे शिक्षण माध्यम के संबंध में उनके द्वारा जारी पत्रों या परिपत्रों को अवैध मानें तथा उन पर कार्रवाई करने या उन्हें लागू करने से बचें;
- विश्वविद्यालय को अपीलकर्ता के पुत्र श्रीकांत के “अंग्रेजी माध्यम कला वर्ग” में प्रवेश का विरोध करने या उस पर रोक लगाने से इंकार करने का निर्देश देना; तथा
- महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को यह निर्देश दिया जाए कि वे श्रीकांत को अंग्रेजी माध्यम में मध्यवर्ती कला कक्षा में इस आधार पर प्रवेश दें कि 1949 के अधिनियम की धारा 4(27), 18(1), 18(14), 38A तथा संविधि 207, 208 तथा 209, साथ ही कुलपति द्वारा जारी पत्र और परिपत्र सभी शून्य और अवैध हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला
गुजरात उच्च न्यायालय ने श्रीकांत के पिता (सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी) द्वारा प्रार्थना के अनुसार 24 जनवरी 1962 के आदेश के माध्यम से रिट जारी की। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया-
- संविधि 207 और 209, वर्तमान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थानों को छोड़कर अन्य संस्थानों में शिक्षा के माध्यम के रूप में और शिक्षण के माध्यम के रूप में गुजराती और/या देवनागरी लिपि में हिंदी को लागू करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें अनधिकृत माना गया और इस प्रकार उन्हें अमान्य घोषित कर दिया गया। यह इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया था कि न तो 1949 के अधिनियम की धारा 4(27) और न ही कोई अन्य प्रावधान विश्वविद्यालय को ऐसे संस्थानों में शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में गुजराती या हिंदी को निर्धारित करने का अधिकार देता है, न ही प्रावधान उसी उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं;
- विश्वविद्यालय को गुजराती या हिंदी को एक माध्यम के रूप में शामिल करने का अधिकार है, लेकिन इसे अन्य भाषाओं को छोड़कर एकमात्र माध्यम नहीं बनाया जा सकता है;
- 1949 के अधिनियम (जैसा कि 1961 में संशोधित किया गया) की धारा 4(27) का परंतुक कहता है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 का उल्लंघन करता है और इस प्रकार, यह राज्य के विधायी अधिकार से परे है। इसलिए, संविधि 207 और 209 शून्य और अमान्य हैं; और
- यदि धारा 4(27) और 1949 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के सही अर्थ में व्याख्या करने पर यह देखा जाता है कि विश्वविद्यालय को अपने संबद्ध महाविद्यालयों के लिए एक विशिष्ट भाषा या भाषाओं को माध्यम के रूप में निर्धारित करने का अधिकार है और उसके पास अपने द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों में उसी उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्ति है, तो एक विशेष भाषा को लागू करने का अधिकार प्रदान करने वाले प्रावधान और उसी को पुष्ट करने वाले संविधि और परिपत्र शून्य होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29(1) और 30(1) का उल्लंघन करेंगे।
उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर गुजरात राज्य और गुजरात विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च न्यायालय में अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिनमें कहा गया कि 1949 के अधिनियम की धारा 4 विश्वविद्यालय को गुजराती और हिंदी को शिक्षण और परीक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने का अधिकार देती है तथा इससे संबंधित सभी प्रावधान वैध हैं। इन अपीलों के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपयुक्तता (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था।
मामले में उठाए गए मुद्दे
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए दो मुद्दे इस प्रकार हैं-
- क्या विश्वविद्यालय अपने संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा और परीक्षा आयोजित करने के लिए गुजराती, हिंदी या दोनों को विशेष भाषा के रूप में लागू कर सकता है?
- क्या विश्वविद्यालय को ऐसी शक्ति प्रदान करने वाली संविधि के परिणामस्वरूप संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 का उल्लंघन होगा?
पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता
विश्वविद्यालय की ओर से वकील ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं-
- धारा 4 के खंड (10)(a) के अनुसार विश्वविद्यालय को क़ानून, अध्यादेश और विनियमों के अनुसार अध्ययन के पाठ्यक्रम स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया था।
- धारा 4(27) विश्वविद्यालय को सशक्त बनाती है, और धारा 18(1)(14) सीनेट को गुजराती, हिंदी या दोनों को शिक्षण और परीक्षा के माध्यम के रूप में आवंटित करने का प्रावधान करने की शक्ति और कर्तव्य प्रदान करती है।
- विश्वविद्यालय के वकील ने भारत सरकार द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों और प्रांतीय सरकारों को 7 अगस्त 1949 को लिखा गया एक पत्र प्रस्तुत किया था। इस पत्र के माध्यम से विभिन्न सिफारिशें की गईं। उनमें से एक है विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर राज्य या प्रांतीय भाषा को लाने का भी अनुरोध किया गया।
- सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूची I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत दी गई शक्ति “समन्वय” और “मानकों का निर्धारण” करने की शक्ति है। समन्वय और निर्धारण शब्दों का अर्थ क्रमशः “मूल्यांकन” और “ठीक करना” है।
- यह भी तर्क दिया गया कि सूची II की प्रविष्टि 11 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा का एक विशेष माध्यम निर्धारित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित तर्क दिए:
- प्रत्यर्थी के वकील ने स्वीकार किया कि राज्य विधानमंडल के पास किसी विश्वविद्यालय को शिक्षण के माध्यम के रूप में कोई भाषा निर्धारित करने का अधिकार है।
- उन्होंने तर्क दिया कि राज्य कानून, जो अंग्रेजी को शिक्षण के माध्यम के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है तथा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ एक क्षेत्रीय भाषा को एकमात्र या अतिरिक्त माध्यम के रूप में उपयोग करने का निर्देश देता है, सूची I की प्रविष्टि 66 का उल्लंघन करता है। ऐसा राज्य कानून राष्ट्रीय आधार पर मानकों और समन्वय के निर्धारण को कठिन या असंभव बना देगा।
- यह भी तर्क दिया गया कि तत्व और सार (पिथ एंड सब्सटेंस) का सिद्धांत तब अप्रासंगिक हो जाता है जब एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि पर निर्भर होती है। ऐसे मामले में, जब मामला एक प्रविष्टि के दायरे से बाहर होता है, तो वह दूसरी प्रविष्टि के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है; इसलिए, कोई अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) नहीं होती है। इससे प्रविष्टियों की व्याख्या के लिए तत्व और सार के सिद्धांत का आह्वान अनावश्यक हो जाता है।
- प्रत्यर्थी ने कहा कि उपर्युक्त मामले में, “प्रत्यक्ष प्रभाव” नामक सिद्धांत लागू होता है, जिसके अनुसार, यदि किसी राज्य कानून का संघ सूची में उल्लिखित प्रविष्टि पर “प्रत्यक्ष प्रभाव” पड़ता है, तो उस राज्य कानून को राज्य सूची के दायरे से बाहर माना जाता है।
- सूची I की प्रविष्टि 66 की व्याख्या के संबंध में यह तर्क दिया गया कि संसद को, कुछ परिस्थितियों में, राज्य कानून द्वारा निर्धारित शिक्षण माध्यम को अपने चुने हुए माध्यम से प्रतिस्थापित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है।
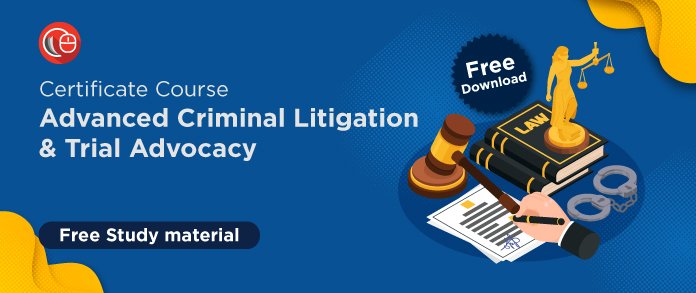
गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर एवं अन्य (1963) में शामिल कानून और अवधारणाएँ
संविधान का अनुच्छेद 254(1)
इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यदि राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया गया है और वह किसी एक के विपरीत है-
- संसद द्वारा बनाया गया कोई प्रावधान या कानून, जो संसद की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है, या,
- समवर्ती सूची (कंकर्रेंट लिस्ट) में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून का कोई प्रावधान,
तब, संसद द्वारा बनाया गया कानून, चाहे वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से पहले या बाद में लागू हुआ हो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून पर प्रबल होगा। इसके अलावा, विरोधाभास की सीमा तक राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भी शून्य माना जाएगा।
सातवीं अनुसूची की तीन सूचियाँ
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच अलग-अलग शक्तियों और कार्यों का आवंटन करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं, अर्थात्,
- सूची I, जिसे संघ सूची के नाम से भी जाना जाता है- इस सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध मामले संघ सरकार, अर्थात् संसद के विशेष अधिकार के अंतर्गत आते हैं। संसद को इसके अंतर्गत उल्लिखित मामलो के संबंध में कानून बनाने का एकमात्र और अनन्य अधिकार है।
- सूची II, जिसे राज्य सूची के नाम से भी जाना जाता है- जैसा कि नाम से पता चलता है और यह संघ सूची की अवधारणा के समान है, राज्य विधानसभाओं को इस सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।
- सूची III, जिसे समवर्ती सूची के नाम से भी जाना जाता है- इस सूची में उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जो संघ और राज्यों के संयुक्त अधिकार क्षेत्र में हैं। यह एक साझा क्षेत्र है और केंद्र तथा राज्य विधानमंडल दोनों ही इन मामलों पर कानून बना सकते हैं।
सूची I की प्रविष्टि 63 से 66
चूंकि प्रविष्टि 63 से 66 वर्तमान मामले से संबंधित हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करने से पहले इन प्रविष्टियों का उल्लेख करना आवश्यक है। प्रविष्टि 63 से 66 में मूलतः कुछ विश्वविद्यालयों और संस्थानों की सूची दी गई है, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व दिया गया है और इसलिए, उनसे संबंधित किसी भी कानून को पारित करने के लिए वे संसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
सूची I की प्रविष्टि 63 में कुछ संस्थाओं का उल्लेख है जो राष्ट्रीय महत्व की हैं; इसमें कहा गया है कि “इस संविधान के प्रारंभ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्थान; अनुच्छेद 371E के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय; संसद द्वारा कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कोई अन्य संस्था।”
प्रविष्टि 64 भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की सूची में जोड़ती है, इसमें कहा गया है कि “वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थान जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं और संसद द्वारा कानून द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए गए हैं।”
प्रविष्टि 65 और 66 में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया गया है जो कानून बनाने की संसद की विशेष शक्ति के अंतर्गत आते हैं।
प्रविष्टि 65 संसद को निम्नलिखित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देती है-
“संघीय एजेंसीज और संस्थाएं-
- पेशेवर, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), जिसमें पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है; या
- विशेष अध्ययन या अनुसंधान को बढ़ावा देना; या
- अपराध की जांच या पता लगाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता।”
प्रविष्टि 66 संसद को “उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में मानकों के समन्वय और निर्धारण” के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देती है।
सूची II की प्रविष्टि 11
प्रविष्टि 11 में उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल को “सूची I की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 तथा सूची III की प्रविष्टि 25 के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा” के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।
यह प्रावधान राज्य विधानमंडल को शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें अपवादों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे कुछ मामलों में संसद को प्राथमिकता मिलती है। हालाँकि, इस प्रविष्टि को अब संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा हटा दिया गया है।
सूची III की प्रविष्टि 25
प्रविष्टि 25 में कहा गया है कि “शिक्षा, जिसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल हैं, सूची I की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अधीन; श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण” के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास है।
सूची II की प्रविष्टि 11 के समान, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें संसद को राज्य विधानसभाओं पर प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित विषयों के संबंध में संघ और राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की साझा शक्ति प्राप्त है।
विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा तैयार किए गए संविधि 207, 208 और 209, जिन्हें 1961 में संशोधित किया गया
गुजरात विश्वविद्यालय ने 1954 में शिक्षण के माध्यम से सुलझने के लिए कुछ नियम बनाए थे। वे संविधि 207, 208 और 209 थे।
संविधि 207
संविधि 207 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है-
- शिक्षा और परीक्षा का माध्यम गुजराती भाषा होगी;
- गुजराती भाषा माध्यम होने के बावजूद, अंग्रेजी भाषा गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 3 के लागू होने की तारीख से अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए माध्यम बनी रहेगी, सिवाय समय-समय पर संविधियो द्वारा अन्यथा प्रदान की जाएगा;
- गुजराती भाषा को माध्यम के रूप में शामिल करने के बावजूद, गैर-गुजराती छात्रों और शिक्षकों के पास माध्यम के रूप में हिंदी भाषा का उपयोग करने का विकल्प होगा। इसके लिए, जब भी आवश्यक होगा, सिंडिकेट इसके विनियमन के लिए उपयुक्त अध्यादेश लागू करेगा।
- उपर्युक्त तीनों बिंदुओं में जो भी उल्लेख किया गया है, उसके बाबजूद, आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के लिए शिक्षण और परीक्षा का माध्यम संबंधित भाषाएं ही होंगी।

संविधि 208
संविधि 208 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है-
- कुछ पाठ्यक्रमों का नाम लिया गया जहां शिक्षण और परीक्षा का माध्यम अब अंग्रेजी नहीं होगा और यह संविधि 207(1) के अनुसार होगा। पाठ्यक्रमों की दो अलग-अलग सूचियों के लिए दो अलग-अलग आवेदन तिथियां प्रदान की गईं।
निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए उपर्युक्त व्यवस्था जून 1955 से लागू होनी थी:
- प्रथम वर्ष कला,
- प्रथम वर्ष विज्ञान, और
- प्रथम वर्ष वाणिज्य।
नीचे उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए यह व्यवस्था जून 1956 से लागू होनी थी:
- इंटर कला इंटर विज्ञान,
- इंटर वाणिज्य (कॉमर्स) और
- प्रथम वर्ष विज्ञान (कृषि)।
- यदि किसी छात्र या शिक्षक को लगता था कि वे गुजराती या हिंदी का उचित प्रयोग नहीं कर सकते तो उन्हें नवंबर 1960 तक अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में प्रयोग करने की अनुमति थी।
संविधि 209
संविधि 209 में कला स्नातक, विज्ञान स्नातक और ऐसी अन्य परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी गई है।
1961 का संशोधन
इसके बाद, गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 के 1961 के संशोधन के साथ, विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा संविधि 207 और 209 में संशोधन किया गया। संशोधित संविधि 207 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है-
- शिक्षा और परीक्षा का माध्यम गुजराती भाषा होगी। नीचे नामित संकायों (फैकल्टी) में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी की अनुमति होगी-
- चिकित्सा संकाय,
- तकनीकी और इंजीनियरिंग संकाय,
- विधि संकाय,
- और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सभी संकाय।
2. अंग्रेजी शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनी रहेगी, लेकिन अध्ययन की अवधि, विषय और पाठ्यक्रम जिसके संबंध में ऐसी छूट दी जाएगी, गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 4(27) के तहत क़ानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
3. जिन विद्यार्थियों और शिक्षकों की मातृभाषा गुजराती नहीं है, उन्हें परीक्षा और शिक्षण के माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग करने का विकल्प दिया जाएगा।
4. संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालय विभागों को एक या अधिक विषयों के लिए हिंदी को माध्यम के रूप में उपयोग करने का विकल्प होगा। यह उन विद्यार्थियों पर लागू होगा जिनकी मातृभाषा गुजराती नहीं है।
5. उपर्युक्त बातों के बाबजूद आधुनिक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के लिए शिक्षण और परीक्षा का माध्यम संबंधित भाषाएं ही होंगी।
संशोधन के बाद, संविधि 209 में कहा गया कि शिक्षण और परीक्षा का माध्यम अब अंग्रेजी नहीं होगा, बल्कि संविधि 207 के अनुसार होगा, जो उसमें उल्लिखित वर्षों से संबंधित परीक्षाओं के साथ प्रभावी होगा।
सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत
“सामंजस्यपूर्ण व्याख्या” का सिद्धांत किसी क़ानून की व्याख्या करने की एक विधि है। यह इस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक क़ानून एक विशिष्ट उद्देश्य और इरादे से तैयार किया गया है और इसे समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए। सरल शब्दों में, यह सिद्धांत यह नियम बनाता है कि जब दो भिन्न विधियों या एक ही विधि के अंतर्गत दो प्रावधानों के बीच कोई विवाद हो, तो न्यायालयों को उनकी व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि उनमें सामंजस्य हो, वे एक साथ लागू रहें तथा किसी भी प्रकार की असंगति से बचा जा सके।
सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।
तत्व और सार का सिद्धांत
“तत्व और सार” का सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है जिसका उपयोग संवैधानिक व्याख्या में किया जाता है। इसका उपयोग संघीय शासन प्रणाली में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अधिनियमित कानून किसकी विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। वाक्यांश “तत्व और सार” का अर्थ है “सच्ची प्रकृति और पदार्थ”।
संघ और राज्य विधानसभाओं को अपने-अपने विषयों पर कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है, जिन्हें संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत अपनी-अपनी सूचियों में विभाजित किया गया है। यदि उनमें से कोई भी दूसरे के विषय का अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो कानून के वास्तविक उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए तत्व और सार के सिद्धांत को लागू किया जाता है। यदि कानून मूलतः उस विषय से संबंधित है जो उसे अधिनियमित करने वाली विधायिका की शक्ति के अंतर्गत आता है, तो उसे शक्ति के अधीन (इंट्रा वायर्स) (कानून बनाने की शक्ति के अंतर्गत) माना जाता है, भले ही वह उसकी शक्तियों से परे मामलों का उल्लंघन करता हो।
इस सिद्धांत के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।
छद्मता का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन)
छद्मता के सिद्धांत का अर्थ है कि विधायिका ने ऐसा करने की शक्ति होने के बहाने कानून बनाया है, हालांकि उसके पास उस विषय के संबंध में कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है। भारत के संविधान में संघ और राज्यों द्वारा कानून बनाने के लिए विषयों का सीमांकन किया गया है। यदि कोई विधायिका इस सीमांकन का उल्लंघन करती है और अपने निर्धारित अधिकार से बाहर कानून बनाती है, तो न्यायपालिका द्वारा इस सिद्धांत का उपयोग ऐसे कार्यों की पहचान करने, कानून की समीक्षा करने और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें शून्य घोषित करने के लिए किया जाता है।
यह सिद्धांत लैटिन कहावत “क्वांडो एलिक्विड प्रोहिबेटर एक्स डायरेक्टो, प्रोहिबेटर एट पेर ओब्लिकम” से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि “जो चीजें सीधे नहीं की जा सकतीं, उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जाना चाहिए”। यह संघ और राज्य विधानसभाओं की विधायी शक्तियों को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इस सिद्धांत को “संविधान पर धोखाधड़ी” के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि विधायिकाएं संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों से परे कार्य करती हैं।
इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।

प्रत्यक्ष प्रभाव का सिद्धांत
प्रत्यक्ष प्रभाव का सिद्धांत एक यूरोपीय कानून-आधारित सिद्धांत है जो लोगों को किसी राष्ट्रीय या यूरोपीय अदालत के समक्ष किसी भी यूरोपीय क़ानून के प्रावधान को लागू करने की अनुमति देता है।
यूरोपीय संघ के न्यायालय ने एनवी अलगेमेन ट्रांसपोर्ट-एक्सपेडाइट ओन्डरनेमिंग वान गेंड एन लूस बनाम नीदरलैंड्स एडमिनिस्ट्रेटी डेर बेलास्टिंगेन (1963) के मामले में पहली बार इस सिद्धांत को तैयार किया। इस मामले में, यूरोपीय न्यायालय ने प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित करने के लिए आवश्यकताएं भी निर्धारित कीं। आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:
- जिस प्रावधान को लागू किया जाना है वह स्पष्ट होना चाहिए;
- प्रावधान में कुछ नकारात्मक दायित्व अवश्य शामिल होना चाहिए;
- यह बिना शर्त होना चाहिए; और
- यह किसी अन्य प्रावधान पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति होने पर, प्रावधान के तहत प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों के समक्ष लागू किया जा सकता है।
प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्धांत के दो पहलू हैं:
- ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) प्रत्यक्ष प्रभाव- इस मामले में, कोई व्यक्ति राज्य के संबंध में यूरोपीय कानून का आह्वान कर सकता है। यदि यूरोपीय कानून का कोई प्रावधान ऊर्ध्वाधर और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी है, तो राज्य या सार्वजनिक निकायों के विरुद्ध कार्रवाई करते समय उस पर भरोसा किया जाता है। ऐसे प्रावधान यूरोपीय कानून और राष्ट्रीय कानून के बीच संबंध से संबंधित हैं।
- क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) प्रत्यक्ष प्रभाव- इस मामले में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में यूरोपीय कानून का आह्वान कर सकता है। यदि यूरोपीय कानून का कोई प्रावधान क्षैतिज और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उस पर भरोसा कर सकता है। ऐसे प्रावधान व्यक्तियों के बीच संबंधों से संबंधित हैं।
मामले से जुड़े पूर्ववर्ती उदाहरण
- हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य (1961)– इस मामले में उड़ीसा खनन क्षेत्र विकास निधि अधिनियम, 1952 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया था। न्यायालय ने सूची II की प्रविष्टियों में प्रयुक्त वाक्यांश “के अधीन” का विश्लेषण किया, जबकि ऐसी प्रविष्टि को सूची I की कुछ अन्य प्रविष्टि के अधीन रखा गया था। इसने माना कि राज्य विधानमंडल को सूची II प्रविष्टि में “अधीन” वाक्यांश द्वारा निहित प्रतिबंध की सीमा तक विधायी शक्ति से वंचित किया गया है।
इस मामले को यह बताने के लिए संदर्भित किया गया था कि, वर्तमान मामले में शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की राज्य की शक्ति प्रतिबंधित है और यह केवल संघ द्वारा प्राप्त शक्तियों की सीमा तक ही है। इसे लागू करते हुए, यह अनुमान लगाया गया कि, यदि कानून का विषय “विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा” के बड़े दायरे में है और यह प्रविष्टि 63 से 66 द्वारा भी शामिल किया गया है, तो संघ को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति रखने वाला माना जाएगा।
2. प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स, खुलना (1947)- न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में, “तत्व और सार” के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए इस मामले का उल्लेख किया था। इस मामले में, विवाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 28 (वचन पत्र) और 38 (बैंकिंग) तथा सूची II की प्रविष्टि 27 (धन उधार) के बीच था। तत्व और सार के सिद्धांत का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया गया था कि क्या बंगाल साहूकार अधिनियम, 1940 राज्य विधानमंडल के लिए अधिकारातीत (अल्ट्रा वायर्स) (कानून बनाने की शक्तियों से परे) था। इस मामले में, न्यायिक समिति ने माना कि अधिनियम का तत्व और सार, अर्थात् इसकी वास्तविक प्रकृति, धन उधार देना है, जो सूची II की प्रविष्टि 27 के अंतर्गत आता है। अत: अधिनियम को वैध माना गया क्योंकि यह अधिनियम संघ की अनन्य शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषयों, अर्थात् सूची I की प्रविष्टि 28 और 38 के अंतर्गत वचन पत्र और बैंकिंग का अतिक्रमण करता है, जो संयोगवश था।
न्यायालय ने संबंधित कानून के तत्व और सार का निर्धारण करने के लिए संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर राज्यों द्वारा उल्लंघन की सीमा पर विचार करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला था। यदि उल्लंघन की सीमा संघ के अधिकार क्षेत्र में है, तो इससे यह संकेत मिल सकता है कि वास्तविक प्रकृति राज्य से संबंधित मामलों से संबंधित नहीं है।
3. बॉम्बे राज्य बनाम एफ. एन. बलसारा (1951)- इस मामले में, मुद्दा बॉम्बे निषेध अधिनियम, 1949 की संवैधानिक वैधता के बारे में था। प्रश्न यह था कि क्या यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 31 (मादक मदिरा – उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री) के अंतर्गत आता है या सूची I की प्रविष्टि 19 (सीमा शुल्क सीमा के पार आयात और निर्यात) के अंतर्गत आता है। तत्व और सार के सिद्धांत की संलिप्तता को मान्य करने के लिए एक तर्क दिया गया, जिसमें कहा गया कि यदि शराब की खरीद, उपयोग, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसका आयात भी प्रभावित होगा। न्यायालय ने इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कथित उल्लंघन कानून की “वास्तविक प्रकृति और चरित्र” को प्रभावित नहीं करता है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम का सार और तत्व सूची II की प्रविष्टि 31 के अंतर्गत आता है, यद्यपि संयोगवश संघ के विधान के दायरे का उल्लंघन हुआ है।
4. ए.एस. कृष्णा बनाम मद्रास राज्य (1957)- इस मामले में, मुद्दा मद्रास निषेध अधिनियम (जिसे अब तमिलनाडु निषेध अधिनियम, 1937 कहा जाता है) की वैधता के बारे में था। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम के प्रावधान उसी मामले से संबंधित मौजूदा भारतीय कानूनों, अर्थात् भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के विरोधाभासी हैं। न्यायालय ने दोहराया कि यदि कोई कानून किसी ऐसे विषय से संबंधित है जो संघ या राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है, तो उसे उस विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में माना जाएगा, भले ही वह विधायी क्षमता से परे के विषयों का अतिक्रमण करता हो। अतिक्रमण की सीमा यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कानून पक्षपातपूर्ण है या नहीं। अन्यथा, अतिक्रमण से कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
5. यूनियन कोलियरी कंपनी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, लिमिटेड, और अन्य बनाम जॉन ब्राइडन (1899) – इस मामले में, मुद्दा यह था कि क्या ब्रिटिश कोलंबिया कोयला खान विनियमन अधिनियम, 1890 की धारा 4 राज्य विधायिका से अधिकारातीत थी। उक्त अधिनियम की धारा 4 में भूमिगत कोयला खदानों में पूर्ण आयु के चीनी लोगो को नियोजित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम, 1867 की धारा 91(25) के अनुसार “नागरिकीकरण और विदेशी” का विषय संघीय संसद के विशेष अधिकार के अधीन था।
प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने यह टिप्पणी की कि यह अधिनियम केवल उन चीनी लोग पर लागू होता है जिन्हें विदेशी या प्राकृतिक नागरिक माना जाता है। इस अधिनियम का इन चीनी लोग को भूमिगत कोयला खदानों में काम करने से रोकने या उन्हें काम करने की अनुमति देने के अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह पूरी तरह से ब्रिटिश कोलम्बिया प्रांत के अधिकार क्षेत्र में था। धारा 91(25) के अनुसार, प्रभुत्व (डोमिनियन) विधानमंडल के पास कनाडा में रहने वाले चीनी लोग के अधिकारों, विशेषाधिकारों और अक्षमताओं से सीधे संबंधित मामलों में विशेष अधिकार था। तत्व और सार के सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने निष्कर्ष निकाला कि संबंधित अधिनियम चीनी लोग के अधिकार और विशेषाधिकारों के बारे में था, जो संसद की विशेष शक्ति के अंतर्गत एक विषय था।
यह निर्णय भी तत्व और सार के सिद्धांत से संबंधित है तथा इसका “प्रत्यक्ष प्रभाव” के सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है।
6. बैंक ऑफ टोरंटो बनाम लैम्बे (1882)– इस मामले में, क्यूबेक अधिनियम, 1774 पर सवाल उठाया गया था। दो मुद्दे उठाए गए थे। पहला यह कि विचाराधीन कर “प्रांत के भीतर कराधान” नहीं था और दूसरा यह कि कर “प्रत्यक्ष कर” नहीं था। न्यायिक समिति ने माना था कि यह अधिनियम प्रांतीय विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है।
7. अल्बर्टा के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) बनाम कनाडा के महान्यायवादी (1939)– इस मामले में, अल्बर्टा प्रांत ने “बैंकों के कराधान” के संबंध में एक अधिनियम पारित किया था। अधिनियम का प्रभाव यह था कि बैंक ऑफ कनाडाको छोड़कर प्रत्येक निगम या संयुक्त स्टॉक कंपनी, जो प्रांत में बैंकिंग या बचत बैंक व्यवसाय करने के लिए निगमित की गई है, पर अन्य क़ानूनों के तहत देय सामान्य कर के साथ-साथ वार्षिक कर भी लगाया जाएगा। इस वार्षिक कर की गणना चुकता पूंजी (पैड-अप कैपिटल) पर आधा प्रतिशत तथा आरक्षित निधि एवं अविभाजित लाभ पर एक प्रतिशत के रूप में की गई थी।
यह माना गया कि लगाया गया कर “प्रांतीय उद्देश्यों के लिए राजस्व जुटाने” के लिए कोई नियमित कराधान नहीं था और, इस प्रकार, इसे ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम की धारा 92(2) के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल की विधायी क्षमता के भीतर कहा जा सकता है, लेकिन यह उन बैंकों के संचालन को रोकने के लिए था जो ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम की धारा 91 के अनुसार संसद के उचित प्राधिकार द्वारा स्थापित किए गए थे।
इस प्रकार, बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि यह अधिनियम कराधान से संबंधित एक क़ानून है, फिर भी यह एक छद्मता का सिद्धांत है जिसका उद्देश्य बैंकिंग संस्थानों के कामकाज को रोकना है, जो प्रभुत्व विधानमंडल के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यह देखा गया कि अधिनियम का तत्व और सार कराधान से संबंधित नहीं था, जो कि ऊपर उल्लिखित धारा 92 के अनुसार प्रांतीय विधानमंडल की शक्ति के अंतर्गत आता था, लेकिन “बैंकिंग” के विषय से संबंधित था, जो प्रभुत्व विधानमंडल की शक्ति के अंतर्गत था। न्यायाधीशों ने किसी विशेष विषय को किस वर्ग, अर्थात् अधिनियम की धारा 91 या धारा 92 के अंतर्गत रखा जाएगा, यह निर्धारित करने में सहायता के लिए कुछ दिशानिर्देश भी तैयार किए। तीन नियम सुझाये गये, जो इस प्रकार हैं:
- धारा 91 और 92 के तहत दी गई दो सूचियों की तुलना यह निर्धारित करने के लिए की जानी है कि संबंधित कानून प्रथम दृष्टया किस दायरे में आता है।
- कानून के प्रभाव की जांच की जानी है, और,
- संबंधित कानून के उद्देश्य या प्रयोजन पर विचार किया जाना है।
8. कलकत्ता गैस कंपनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1962)- इस मामले में, मुद्दा ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, 1960 को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधायिका की क्षमता के बारे में था। न्यायालय ने कहा था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान की गई तीन सूचियाँ पृथक (सेपरेट) विधानमंडलों के कार्य-क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाले सीमांकित क्षेत्र हैं। सूचियों के अंतर्गत प्रविष्टियों की भाषा को प्राथमिकता दी जानी है, लेकिन इसमें अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) या प्रत्यक्ष संघर्ष के मामले हो सकते हैं। ऐसे मामलों में, उनकी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करना न्यायालय का कर्तव्य है। न्यायालय ने कहा था कि यह एक सुस्थापित नियम है कि परस्पर विरोधी प्रविष्टियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, भले ही वे एक ही सूची से संबंधित हों या विभिन्न सूचियों से संबंधित हों।
9. ड्यूचर बनाम गैस लाइट एंड कोक कंपनी (1925)– इस मामले में, यह माना गया कि, जब किसी निगम का गठन विधान द्वारा किया जाता है, तो अधिनियम के प्रयोजनों पर विचार करते हुए तथा इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए, निगम द्वारा अपनाए जाने वाले उद्देश्य अधिनियम पर आधारित होने चाहिए तथा शक्तियां भी अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या युक्तिसंगत निहितार्थ द्वारा प्रदान की जानी चाहिए।

मामले का फैसला
गुजराती या हिंदी या दोनों को विशेष माध्यम के रूप में लागू करना
धारा 4 और इसके अंतर्गत खंड
इस संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1949 अधिनियम की धारा 4 के कुछ खंडों पर विचार किया। विशेष खंड और उनसे निकाले गए निष्कर्ष आसानी से समझने के लिए नीचे अलग-अलग बिंदुओं में सूचीबद्ध हैं:
- खंड (1)- 1949 के अधिनियम में मूल रूप से इस खंड के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान निहित थे:
“ऐसी शिक्षा शाखाओं और अध्ययन पाठ्यक्रमों में अनुदेशन (इंस्ट्रक्शन), अध्यापन और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, जैसा कि वह अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के लिए व्यवस्था करना उचित समझता है”
वर्तमान अधिनियम, जिसे 2016 तक संशोधित किया गया है, खंड (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान करता है:
“पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित अनुदेश की व्यवस्था करना, शिक्षा की ऐसी शाखाओं और अध्ययन पाठ्यक्रमों में अध्यापन और प्रशिक्षण प्रदान करना, जिन्हें वह उचित समझे, अनुसंधान, उन्नति और ज्ञान के प्रसार के लिए प्रावधान करना और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष स्नातक पाठ्यक्रम संचालित करना”
सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की इस राय से सहमत नहीं था कि खंड (1) के तहत शक्ति केवल विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्थानों तक ही सीमित है तथा संबद्ध महाविद्यालय इसके दायरे में नहीं आते हैं। प्रावधान की भाषा इस प्रतिबंध का समर्थन नहीं करती है। हालाँकि, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस कथन पर सहमति व्यक्त की कि यह शक्ति शिक्षण के माध्यम से संबंधित नहीं है, बल्कि विभिन्न शाखाओं और पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम से संबंधित है।
यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस धारा के अनुसार, विश्वविद्यालय शाखाओं और पाठ्यक्रमों में निर्देश, शिक्षण और प्रशिक्षण का निर्देशन कर सकता है, लेकिन यह ऐसे निर्देश देने के लिए एक विशेष माध्यम प्रदान नहीं करता है।
2. खंड (2) – “ऐसा प्रावधान करना जिससे संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों को अध्ययन में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिले”
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस खंड का शिक्षण के विशिष्ट माध्यम के विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. खंड (7) – 2016 तक संशोधित अधिनियम, इस प्रावधान को वर्तमान में खंड (10) में रखता है। प्रावधान में कहा गया है:
“विभिन्न परीक्षाओं के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित करना”
इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह खंड शिक्षा का एक विशेष माध्यम निर्धारित करने से संबंधित नहीं है।
4. धारा (8) – नवीनतम संशोधित अधिनियम के अनुसार, यह प्रावधान अब उसी धारा के अंतर्गत धारा (9) में निहित है। प्रावधान में कहा गया है कि:
“महाविद्यालयो, विश्वविद्यालय विभागों, विश्वविद्यालय केंद्रों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान कार्य का मार्गदर्शन करना”
इस प्रावधान में भी संशोधन किए गए हैं, लेकिन चूंकि इस खंड का भी किसी विशिष्ट माध्यम को लागू करने की शक्ति से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि न्यायालय ने कहा है, इसलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं।
5. खण्ड (10) – यह ध्यान देने योग्य है कि इस खण्ड में निहित प्रावधान को नवीनतम संशोधन के अनुसार खण्ड (12) में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रावधान में कहा गया है कि:
“परीक्षा आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को डिग्री, उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक सम्मान प्रदान करना जो
-
- विश्वविद्यालय या किसी संबद्ध महाविद्यालय में अनुमोदित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जब तक कि उसे संविधियो, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से छूट न दी गई हो और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या
- अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत अनुसंधान किया हो”
नवीनतम संशोधित अधिनियम के अनुसार इस खंड में थोड़ा परिवर्तन किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय की इस दलील को खारिज कर दिया था कि धारा 10(a) स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय को अपनी पसंद की एक विशिष्ट भाषा को विशिष्ट माध्यम के रूप में लागू करने की शक्ति प्रदान करती है, जो इस मामले में गुजराती, हिंदी या दोनों थी। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसा प्रावधान अपने आप में ऐसा सशक्तीकरण प्रदान नहीं करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फिर भी, विश्वविद्यालय के पास ऐसे व्यक्तियों को डिग्री या शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने का अधिकार है, जिन्होंने अनुमोदित पाठ्यक्रम पूरा किया हो तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों।
6. खंड (14)- प्रावधान को अब खंड (20) के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है और यह निम्नलिखित प्रावधान करता है:
“महाविद्यालयो, मान्यता प्राप्त संस्थानों और अनुमोदित संस्थानों का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें अनुदेशन, शिक्षण और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाए रखे जाएं तथा उनमें पर्याप्त पुस्तकालय और प्रयोगशाला प्रावधान किए जाएं”
संक्षेप में, इस प्रावधान में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाए रखे जाएं। इसलिए, इसका किसी विशिष्ट माध्यम के अनुदान से कोई संबंध नहीं है।
7. खण्ड (15)- इस खण्ड को अब खण्ड (24)(a) के अन्तर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है। इस खंड के माध्यम से विश्वविद्यालय को यह अधिकार दिया गया है:
“संबद्ध महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त संस्थानों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वयित करना तथा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना।”
हालाँकि, यह स्पष्ट है कि खंड में शिक्षण और परीक्षा का एक विशेष माध्यम लागू करने की किसी शक्ति का उल्लेख नहीं है, जैसा कि विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था।
8. खंड (27)- असंशोधित खंड में निम्नलिखित उल्लेख है:
“देवनागरी लिपि में गुजराती और हिंदी के अध्ययन के विकास को बढ़ावा देना तथा शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में गुजराती या देवनागरी लिपि में हिंदी या दोनों का उपयोग करना।
बशर्ते कि अंग्रेजी ऐसे विषयों में शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनी रहेगी और धारा 3 के लागू होने की तारीख से दस वर्ष से अधिक की अवधि तक, जैसा कि समय-समय पर संविधियो द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान की व्याख्या “प्रचार” शब्द को महत्व देने के रूप में की, इस प्रकार कहा कि विश्वविद्यालय को इन भाषाओं के उपयोग को “प्रचारित” करने की शक्ति दी गई थी। विश्वविद्यालय के पास इन विशेष भाषाओं के अध्ययन और माध्यम के रूप में उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करने की शक्ति थी, लेकिन उसे उन्हें शिक्षण और परीक्षा का एकमात्र माध्यम बनाने की शक्ति नहीं दी गई थी।
पुनः, “शिक्षा और परीक्षा के माध्यम के रूप में” उपपद में “ए” के उपयोग पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि विधायिका का इरादा गुजराती या हिंदी को शिक्षा के माध्यमों में से एक बनाने का था। स्पष्टतः ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि ऐसी शक्ति का सृजन किया जाए जिसके माध्यम से गुजराती या हिंदी को शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाया जा सके। यह बात खंड के परंतुक में “अंग्रेजी शिक्षा और परीक्षा का माध्यम बनी रह सकती है” वाक्यांश में “द” के प्रयोग से समर्थित होती है।
इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि परंतुक से पता चलता है कि विधायिका पहले से मौजूद शिक्षा और परीक्षा के एकमात्र माध्यम, अर्थात अंग्रेजी को जारी रखना चाहती थी।

अंत में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि, प्रावधान के अनुसार, अंग्रेजी को कुछ विषयों के संबंध में शिक्षण के माध्यम के रूप में जारी रखना था और, खंड के सक्रिय भाग के अनुसार, माध्यम के रूप में गुजराती और हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना था। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गुजराती या हिंदी को एकमात्र माध्यम के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना था, बल्कि अंग्रेजी के साथ-साथ शिक्षण और परीक्षा के लिए भी इसे अपनाया जाना था।
9. खंड (28) – न्यायालय द्वारा उल्लिखित असंशोधित संस्करण (वर्जन) है:
“विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तथा सामान्य रूप से कला, विज्ञान और शिक्षा तथा संस्कृति की अन्य शाखाओं को विकसित करने तथा बढ़ावा देने के लिए पूर्वोक्त शक्तियों के अनुरूप या उससे परे सभी कार्य और चीजें करना”
यह प्रावधान विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को और आगे बढ़ाने के लिए है। यह खंड, खंड (27) के साथ मिलकर काम करता है। यह निष्कर्ष निकालना खंड (27) पर निर्भर करता है कि क्या इस खंड की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि विश्वविद्यालय के उद्देश्य को बढ़ावा मिले कि गुजराती या हिंदी को शिक्षा और परीक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में लागू किया जाए।
धारा 18 और इसके अंतर्गत शक्तियां और कर्तव्य
सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के इस तर्क पर विचार किया कि धारा 18 के तहत विश्वविद्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार, सीनेट को शिक्षण और परीक्षा के माध्यम के रूप में गुजराती या हिंदी या दोनों के उपयोग के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति थी। इस संबंध में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि, स्पष्टतः, उल्लिखित विभिन्न खंडों की भाषा यह अर्थ प्रदान नहीं करती है कि खंड विश्वविद्यालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सीनेट को अधिकृत करने के साथ-साथ एक अतिरिक्त कर्तव्य भी प्रदान करते हैं। हालाँकि, न्यायालय ने यह मान्यता स्वीकार कर ली कि सीनेट की प्रत्येक शक्ति का एक संगत कर्तव्य भी है, लेकिन उसने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि गुजराती, हिंदी या दोनों को माध्यम के रूप में उपयोग करने से संबंधित शक्ति में इसे शिक्षण और परीक्षा का एकमात्र माध्यम बनाने का कर्तव्य भी शामिल है। प्रावधान में “शिक्षण और परीक्षा के माध्यम के रूप में” वाक्यांश में “ए” का प्रयोग यह इंगित करता है कि इन भाषाओं का प्रयोग मौजूदा अनेक माध्यमों के अतिरिक्त होगा न कि एकमात्र माध्यम होगा। इसके अलावा, धारा 18, 20 या 22 के किसी अन्य प्रावधान का उल्लेख पक्षों द्वारा नहीं किया गया, जो विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगों को विभिन्न शक्तियां और कर्तव्य प्रदान करते हैं और न्यायालय को ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं मिला, जो विश्वविद्यालय के अंगों को गुजराती या हिंदी को शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में लागू करने का अधिकार देता हो।
न्यायालय ने यह भी कहा कि संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम उपलब्ध कराने की शक्ति में अनिवार्य रूप से शिक्षण और परीक्षा का एक विशेष माध्यम लागू करने की शक्ति शामिल नहीं है।
भारत सरकार की सिफारिश
याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय ने 7 अगस्त 1949 के एक पत्र का हवाला दिया था, जो भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को लिखा गया था। उस पत्र में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा के लाभ के लिए कुछ सिफारिशें की थीं और विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को समय पर उनका क्रियान्वयन (इंप्लीमेंट) करने का निर्देश दिया था। अनुशंसित सात मामलो में से दो पर इस मामले में चर्चा की गई, जो इस प्रकार थीं:
- विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे आने वाले पांच वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण और परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर राज्य, प्रांत या क्षेत्र की भाषा को धीरे-धीरे लागू करने के लिए कदम उठाएं, और,
- विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वे प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान संघीय भाषा में अनिवार्य परीक्षा आयोजित करें तथा उन विद्यार्थियों के लिए संघीय भाषा में शिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करें जो इसे वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना चाहते हैं।
न्यायालय ने कहा कि यद्यपि भारत सरकार ने 1949 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षण और परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से उसके स्थान पर एक क्षेत्रीय भाषा को लाने के लिए उपर्युक्त सिफारिशें प्रस्तावित की थीं, लेकिन इसे प्रावधानों की इस तरह से व्याख्या करने का उचित कारण नहीं माना जा सकता है जो स्पष्ट रूप से व्यक्त विधानमंडल की मंशा के विपरीत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिकांश विश्वविद्यालयों द्वारा इन सिफारिशों की अवहेलना की गई। 1949 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लेख किया गया था कि जैसा कि समिति ने सुझाव दिया था, अधिनियम विश्वविद्यालय को गुजराती या हिंदी, जो राष्ट्रीय भाषा है, को शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाने का अधिकार देता है। केवल उन विषयों को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया गया जिनमें अंग्रेजी माध्यम आवश्यक माना गया था। ऐसे विषयों में पहले दस वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में अनुमति दी गई थी।
यह कहा गया कि, विधानमंडल द्वारा शामिल किए गए किसी प्रत्यक्ष प्रावधान के अभाव में, उद्देश्य और कारण कथन में उल्लिखित सरकार का प्रस्ताव यह मानने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा कि ऐसे प्रस्ताव को प्रभावी किया गया है। उद्देश्य और कारण किसी क़ानून के अधिनियमन के पीछे के कारण को निर्दिष्ट करते हैं, लेकिन क़ानून की व्याख्या के मामलों में, उद्देश्य और कारणों की उपेक्षा की जानी चाहिए।
इस संबंध में अंतिम निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि, जब धारा 4(27) का प्रभावी भाग विश्वविद्यालय को गुजराती या हिंदी को शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में लागू करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, तो इसे 1961 के संशोधन द्वारा संशोधित प्रावधान द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किया गया नहीं कहा जा सकता है। यह प्रावधान केवल कुछ पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग को दस वर्ष की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाने की घोषणा करता है। परंतुक में विधानमंडल द्वारा निश्चित उपपद (आर्टिकल) “द” के प्रयोग पर भी प्रकाश डाला गया है, जब इरादा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में चित्रित करना था, तथा अनिश्चित उपपद “ए” के प्रयोग पर भी प्रकाश डाला गया है, जब इरादा भाषा को शिक्षा के अनेक माध्यमों में से एक के रूप में चित्रित करना था।
इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि न तो असंशोधित अधिनियम और न ही संशोधित अधिनियम विश्वविद्यालय को ऐसी कोई शक्ति प्रदान करता है कि वह गुजराती, हिंदी या दोनों को शिक्षा और परीक्षा के एक विशेष माध्यम के रूप में लागू कर सके। इस प्रकार, सीनेट ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि सीनेट एक निकाय है जो विश्वविद्यालय की ओर से कार्य करता है और उसके पास केवल वे ही शक्तियां हैं जो अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों के दायरे में आती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से सहमति जताते हुए निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी खंड के तहत गुजराती, हिंदी या दोनों भाषाओं को शिक्षा और परीक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में लागू करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।
सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 66 का उल्लंघन
सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची II की प्रविष्टि 11 के सामंजस्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकता
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 17, बम्बई राज्य विधानमंडल को 1949 का अधिनियम पारित करने का अधिकार देती है। प्रविष्टि 17 में कहा गया है, “शिक्षा के अंतर्गत सूची I के परिच्छेद (पैराग्राफ) 13 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अलावा अन्य विश्वविद्यालय भी शामिल हैं।”
सूची I के परिच्छेद 13 में दो विश्वविद्यालयों का उल्लेख है, अर्थात् बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इस प्रकार, राज्य विधानमंडल को उक्त दो विश्वविद्यालयों को छोड़कर शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। “शिक्षा” शब्द इतना व्यापक है कि इसमें सभी संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान लिया कि राज्य विधानमंडल के पास भी विश्वविद्यालय में संघीय या किसी क्षेत्रीय भाषा को विशेष माध्यम के रूप में लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। न्यायालय ने कहा कि यदि धारा 4(27) द्वारा राज्य विधानमंडल विश्वविद्यालय को किसी भाषा को शिक्षण के विशेष माध्यम के रूप में निर्धारित करने का अधिकार देता है, तो संविधि 207, 208 और 209 की वैधता के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। हालाँकि, धारा 4(27) विश्वविद्यालय को गुजराती या हिंदी भाषा को शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में लागू करने का अधिकार नहीं देती है।
भारतीय संविधान ने संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच शिक्षा के विषय में विधायी शक्तियों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत “उच्च, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और श्रमिकों के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण” के संबंध में कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति का उल्लेख अब सूची II की प्रविष्टि 11 के तहत किया गया है और इसे भारत के संविधान के तहत पांच प्रविष्टियों, अर्थात् सूची I के तहत प्रविष्टि 63 से 66 और सूची III के तहत प्रविष्टि 25 के अधीन किया गया है। सूची I की प्रविष्टि 63 से 66 में शिक्षा विषय से संबंधित उन मामलों का उल्लेख है जो संसद की अनन्य विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने सूची II की प्रविष्टि 11 में प्रयुक्त वाक्यांश “के अधीन” पर ध्यान दिया, जो सूची I की प्रविष्टि 63 से 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 को राज्य विधानमंडल के कानून के दायरे से बाहर रखता है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि राज्य विधानमंडल के पास शिक्षा से संबंधित मामलों के संबंध में सीमित शक्ति है।
न्यायालय ने पक्षों की इस दलील को खारिज कर दिया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के माध्यम या को निर्धारित करने वाले कानून हमेशा सूची II की प्रविष्टि 11 के दायरे में आते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है और इसका पालन किया जाता है, तो धारा 63 से 66 तक की अपवर्जित प्रविष्टियों के लिए भी शिक्षण माध्यम पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास रहेगी, लेकिन अपवर्जित प्रविष्टियों के अन्य क्षेत्रों के लिए, शिक्षण माध्यम के अलावा, कानून बनाने की शक्ति संघीय संसद के पास बनी रहेगी। इस व्याख्या से ऐसे बेतुके परिणाम सामने आएंगे कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों के लिए भी शिक्षा के माध्यम से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होगी, हालांकि उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों के संबंध में उनके पास कोई अन्य शक्ति नहीं होगी।
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने सुझाव दिया कि सूची II की प्रविष्टि 11 और सूची I की प्रविष्टि 66 का सामंजस्यपूर्ण निर्माण किया जाना चाहिए। यह स्वीकार किया गया कि दोनों प्रविष्टियाँ एक-दूसरे से अतिव्यापी हो रही हैं, लेकिन प्रतिच्छेद की स्थिति में, सूची I की प्रविष्टि 66 को सूची II की प्रविष्टि 11 द्वारा सौंपी गई राज्य शक्ति पर प्राथमिकता दी जानी है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि राज्य विधानमंडल को प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है, जिसमें शिक्षा के माध्यम के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है। दूसरी ओर, प्रविष्टि 63 से 66 के अनुसार, राष्ट्रीय या विशेष महत्व के संस्थान और उच्च शिक्षा संस्थान संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए, शिक्षा के माध्यम के संबंध में कानून बनाने की शक्ति भी संघ में निहित है।

संघ विधानमंडल की अधिभावी (ओवरराइडिंग) शक्ति
न्यायालय ने कहा कि, यद्यपि राज्य के पास केवल प्रविष्टि 66 में उल्लिखित संस्थानों में पाठ्यक्रम और अध्ययन के पाठ्यक्रम तय करने की शक्ति है, जिसमें शिक्षण का माध्यम तय करना भी शामिल है, तथापि संघ की संसद सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। संघीय संसद को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्यक्रम, और शिक्षण माध्यम शिक्षा के मानक को बनाए रखें तथा राष्ट्रीय आधार पर मानकों के समन्वय को सुगम बनाएं। यद्यपि विधानमंडलों की शक्तियों की अलग-अलग सूचियां हैं, फिर भी कुछ हद तक उनमें अधिव्यापन होना अपरिहार्य है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस संबंध में उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक सामान्य परीक्षण निर्धारित करना संभव नहीं है। इस प्रकार, यह अतिव्यापी इस प्रकार मौजूद है कि, किसी राज्य के अंदर, राज्य विधानमंडल के पास पाठ्यक्रम, और शिक्षण माध्यम निर्धारित करने की शक्ति होगी, जबकि केंद्र सरकार के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति भी नहीं होगी कि मानकों को पूरा किया जाए, उन्हें बनाए रखा जाए और उनमें सुधार किया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर किया गया एक अन्य बिन्दु यह था कि, भले ही संघ ने अपनी शक्तियों की पूरी क्षमता तक कानून नहीं बनाया हो, फिर भी राज्य को ऐसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं प्राप्त है जो संविधान के अंतर्गत संघ के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां तक कि संघ और राज्य विधानमंडलों को आवंटित पृथक मामलों में भी, दोनों विधानमंडलों की पृथक अनन्य शक्तियों के अंतर्गत अधिनियमित कानून हो सकते हैं, जिनके प्रावधान एक-दूसरे के विरोधाभासी हों। संघर्ष के ऐसे मामलों में, “तत्व और सार” के सिद्धांत को संबंधित कानून पर लागू किया जाना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि किस विधायिका के पास सर्वोच्चता है। राज्य कानून की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या यह प्रविष्टि 66 के तहत “मानक के समन्वय और निर्धारण” को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, न्यायालय ने उल्लेख किया था कि राज्य विधानमंडल ऐसे संस्थानों में शिक्षा पर कानून बना सकता है जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं, अर्थात जिन्हें सूची I की प्रविष्टि 64 में शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि, राज्य विधानमंडल का यह अधिनियम प्रविष्टि 66 के तहत “मानक के समन्वय और निर्धारण” को प्रभावित करने के अधीन होगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254(1) इस तर्क का समर्थन करता है कि संघीय कानून, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से श्रेष्ठ है। इस प्रकार, यदि संघ और राज्य दोनों समन्वय और मानकों के निर्धारण के संबंध में कानून बनाते हैं, तो संघ द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता दी जाएगी। यहां तक कि यदि संघीय संसद ने अनन्य संघ सूची में उल्लिखित किसी विषय पर कानून नहीं बनाया है, तो राज्य को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। फिर भी, यदि राज्य विधानमंडल संघ सूची से संबंधित विषय पर कोई कानून बनाता है, तो ऐसा कानून अवैध माना जाएगा।
सूची I की प्रविष्टि 66 की व्याख्या
न्यायालय ने सूची I की प्रविष्टि 66 के संबंध में विश्वविद्यालय के वकील द्वारा सुझाई गई व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। यह कहा गया कि जब तक स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया जाए या कोई आवश्यकता न हो, प्रविष्टि 66 की संकीर्ण एवं प्रतिबंधित व्याख्या की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी मामले पर कानून बनाने की शक्ति में वे सभी संबंधित पहलू शामिल हैं, जिनके बारे में तर्कपूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि वे उस मामले में शामिल हैं। प्रविष्टि 66 या भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि प्रविष्टि 66 में “समन्वय” का अर्थ केवल “मूल्यांकन” है। सामान्यतः, “समन्वय” शब्द का अर्थ संतुलन या सामंजस्य स्थापित करना होता है। इस प्रकार, समन्वय की शक्ति न केवल मूल्यांकन करने की शक्ति है, बल्कि किसी चीज़ को सामंजस्य या संतुलित करने की शक्ति भी है। इसके अलावा, सूची I की प्रविष्टि 66 द्वारा प्रदत्त शक्ति किसी आपातस्थिति या अक्षम मानकों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं है, जिसके लिए ऐसी शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होती है।
न्यायालय ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में “मानकों के समन्वय और निर्धारण” के संबंध में कानून बनाने की शक्ति में मानकों में विसंगतियों को रोकने और दूर करने की शक्ति भी शामिल है। इस प्रावधान के माध्यम से भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य समन्वय को अधिकृत करना तथा ऐसे समन्वय की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाली किसी भी स्थिति के अस्तित्व को रोकना था। न्यायालय ने आगे इस शक्ति को पूर्ण एवं बिना शर्त के रूप में परिभाषित किया।
“शिक्षण माध्यम” की अवधारणा को दोनों प्रविष्टियों अर्थात सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची II की प्रविष्टि 11 में अलग-अलग शामिल किया गया है। जब इसे प्रविष्टि 66 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, तो यह प्रविष्टि 11 के अपवर्जित भाग के अंतर्गत आएगा। शिक्षा के मानक को बनाए रखने में “शिक्षण माध्यम” की भूमिका इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षण प्रदान करने के लिए माध्यम का चयन कितना महत्व रखता है। न्यायालय ने इस मामले को यह कहते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई कानून किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को शिक्षण के माध्यम के रूप में लागू करता है, भले ही कोई अध्ययन सामग्री, शिक्षण संकाय या यहां तक कि विषयों को समझने में असमर्थ छात्र न हों, तो यह मानकों को कम कर देगा, और फिर कानून सूची I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आ जाएगा और सूची II की प्रविष्टि 11 के तहत दी गई शक्ति से बाहर हो जाएगा।
धारा 4(27) में संशोधन
सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 4(27) के संशोधित प्रावधान को इस आधार पर अवैध घोषित करने में उच्च न्यायालय से असहमति जताई कि यह राज्य की विधायी शक्ति के दायरे से बाहर है। न्यायालय ने दोहराया कि संशोधित प्रावधान का उद्देश्य कुछ चयनित विषयों में दस वर्ष की निर्धारित अवधि से आगे भी शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति देना था। 1949 के अधिनियम के लागू होने से पहले विश्वविद्यालयों में सभी विषयों के लिए अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम थी। इस प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय को चयनित विषयों में शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति देने का अधिकार दिया गया। यह संशोधन पहले से मौजूद माध्यम के अलावा किसी अन्य विशिष्ट माध्यम को लागू करने की शक्ति को अवरुद्ध करता है।
अधिनियम से पहले पूरे देश में शिक्षा का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी था। यह कहा गया कि शिक्षण के एक सामान्य माध्यम के अस्तित्व से मानकों में कमी नहीं आ सकती तथा मानकों के समन्वय और निर्धारण पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। संशोधन का उद्देश्य विशिष्ट विषयों के लिए अंग्रेजी को माध्यम के रूप में जारी रखने की अनुमति देना था और इसे सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत संघ की शक्तियों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।
यदि विश्वविद्यालय के पास शिक्षण का विशिष्ट माध्यम लागू करने की शक्ति नहीं है, तो 1949 के अधिनियम की धारा 38A भी निस्संदेह अवैध नहीं होगी।
गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उसने संविधि 207 और 209 को अवैध घोषित किया था, जहां तक वे गुजराती, हिंदी या दोनों को शिक्षा के एकमात्र माध्यम के रूप में लागू करने से संबंधित हैं।
उच्च न्यायालय द्वारा धारा 4(27) और धारा 38A को अवैध घोषित करने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति सुब्बा राव की असहमतिपूर्ण राय
असहमतिपूर्ण राय न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने दी थी। तत्व और सार के सिद्धांत की प्रासंगिकता पर चर्चा करने के अलावा, उन्होंने दो मुद्दों पर विचार किया, जो निम्नलिखित हैं:
- क्या राज्य विधानमंडल को भारत के संविधान के तहत ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जो संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा का एक विशेष माध्यम निर्धारित करता हो, और
- क्या विश्वविद्यालय को 1949 के अधिनियम, जिसे 1961 में संशोधित किया गया था, के अंतर्गत शिक्षण का विशिष्ट माध्यम लागू करने की शक्ति प्राप्त है।
तत्व और सार के सिद्धांत की प्रासंगिकता
न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि सार और तत्व का सिद्धांत अप्रासंगिक है जब एक प्रविष्टि दूसरी प्रविष्टि पर सशर्त है और दोनों प्रविष्टियाँ अलग-अलग सूचियों के अंतर्गत हैं। इसके बजाय, उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में, कानून का एक हिस्सा एक प्रविष्टि के दायरे से बाहर कर दिया गया है और उसे दूसरी प्रविष्टि में शामिल कर दिया गया है। इसका प्रभाव वैसा ही है जैसा दो प्रविष्टियों को अलग-अलग सूचियों में रखने से होता है। सार और तत्व के सिद्धांत का अर्थ है कि यदि कानून का सार किसी विशेष विधायिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उसे वैध माना जाएगा, भले ही वह कानून उस विधायिका के दायरे से बाहर के मामलों तक विस्तारित हो। कानून का वास्तविक चरित्र चिंता का विषय है तथा अन्य प्रविष्टियों पर किसी भी संयोगवश उल्लंघन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति ने इस संपूर्ण चर्चा का सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा कि, जब प्रश्न उस शक्ति के दायरे का हो जिसके अंतर्गत कानून आता है, तो न्यायालय को कानून के दायरे, प्रभाव, सार और तत्त्व पर निर्णय करना होता है। यदि कोई राज्य कानून किसी केंद्रीय विषय के अधिकार क्षेत्र का इतना अधिक अतिक्रमण करता है कि वह केंद्रीय अधिकार क्षेत्र को गंभीर रूप से सीमित कर देता है, तो यह निष्कर्ष निकालना होगा कि राज्य कानून एक छद्मता का सिद्धांत है तथा अपने सार-तत्व में यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, न कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है।

भारत के संविधान के तहत राज्य विधानमंडल को विशेष माध्यम निर्धारित करने वाले कानून बनाने का अधिकार
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने कहा कि सूची II की प्रविष्टि 11 के अनुसार शिक्षा का संपूर्ण क्षेत्र राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। केवल सूची I की प्रविष्टियाँ 63 से 66 ही अपवाद के रूप में उल्लिखित हैं। शिक्षण माध्यम शिक्षा का एक अविभाज्य घटक है, क्योंकि इसके बिना शिक्षा संभव नहीं है; यह वह तरीका है जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती है। यह उचित नहीं है कि शिक्षा के माध्यम का विषय संसद के अधिकार के अंतर्गत दिया जाए और शिक्षा से संबंधित शेष विषय-वस्तु राज्य को सौंप दी जाए।
यह एक तथ्य है कि विशिष्ट विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम सूची I की प्रविष्टि 63 में शामिल है। साथ ही, विश्वविद्यालय शिक्षा से शिक्षा के माध्यम को बाहर करने का कोई कारण नहीं है, जैसा कि सूची II की प्रविष्टि 11 के तहत उल्लिखित है। यह भी नोट किया गया कि सूची I की प्रविष्टि 66 में प्रथम दृष्टया शिक्षण माध्यम का विषय स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
अपीलकर्ता पक्ष द्वारा “समन्वय” और “मानकों का निर्धारण” शब्दों की व्याख्या को प्रतिबंधात्मक माना गया और यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता तो संसद इस परिदृश्य से पूरी तरह बाहर हो जाती। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत व्याख्या राज्य प्रविष्टि को बुरी तरह प्रभावित करने वाली मानी गई, जिसे तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रविष्टि 11 की भाषा स्पष्ट और सटीक न हो।
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने कहा कि “निर्धारित करना” का अर्थ है “निपटान करना, निर्णय लेना या तय करना” और “समन्वय” का अर्थ है “एक दूसरे के सापेक्ष उचित स्थिति में एक ही क्रम, रैंक या डिवीजन में रखना और जिस प्रणाली का वे हिस्सा हैं, उसके लिए रखना; किसी विशेष परिणाम के उत्पादन के लिए संयुक्त क्रम में कार्य करना” है।
प्रविष्टि 66 संसद को उच्च शिक्षा संस्थानों में “मानकों के निर्धारण” के लिए कानून बनाने का अधिकार देती है। इससे संस्थानों में सामंजस्यपूर्ण समन्वय स्थापित होगा, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार होने की आशा है। यह भी देखा गया कि ऐसे मानकों को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष शिक्षण माध्यम का होना आवश्यक नहीं है।
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने चर्चा की कि शिक्षा के कई घटक हैं और जब “शिक्षा” शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सभी शामिल हो जाते हैं। यदि घटकों को “मानकों का समन्वय और निर्धारण” शीर्षक के अंतर्गत रखा जाए, तो “शिक्षा” की प्रविष्टि बिना विषय-वस्तु के रह जाएगी। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को लागू करना तथा राज्य विधानमंडलों और संघ विधानमंडल की शक्ति और हस्तक्षेप की सीमा के बीच सीमांकन करना आवश्यक है। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए कानून बना सकता है। दूसरी ओर, संसद को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब समन्वय में सहायता के लिए ऐसे मानकों में सुधार की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, संसद बेहतर सुविधाएं प्रदान करने, सामान्य मानकों को उन्नत करने, आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने आदि के लिए कानून बना सकती है, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालय के मानकों को बढ़ाना है।
संसद ऐसा कानून भी बना सकती है जो शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाई गई भाषा में सुधार करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ताकि इसे उच्च शिक्षा और तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक उपयोगी साधन बनाया जा सके। भले ही इस तरह के कानून का सार और तत्व “मानकों का समन्वय और निर्धारण” हो, लेकिन शिक्षण के माध्यम को शामिल करना बाधा नहीं माना जाएगा क्योंकि सुधार का उद्देश्य मौजूद है। लेकिन “समन्वय” की आड़ में पूर्ण विस्थापन की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसे मामले में शिक्षा के विषय पर सीधा उल्लंघन होता है।
सूची I की प्रविष्टि 66 किसी ऐसे प्रावधान को लागू करने की अनुमति नहीं देती है जिसके परिणामस्वरूप किसी बाहरी संगठन द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है, यह ऐसे बाहरी निकाय को मानकों को निर्धारित करने और उन मानकों तक पहुंचने में सहायता करने की अनुमति देता है।
शिक्षा के माध्यम के संबंध में भारतीय संविधान की योजना
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय संविधान भी संसद को शिक्षा के माध्यम के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देने के खिलाफ है। जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब कई क्षेत्रीय भाषाएं थीं, जिनका उल्लेख आठवीं अनुसूची में भी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम होने के साथ-साथ प्रशासन की आधिकारिक भाषा भी थी। इरादा यह था कि अंग्रेजी को सभी स्तरों पर प्रतिस्थापित किया जाए लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का उल्लेख किया गया, जो देवनागरी लिपि में हिन्दी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। इसके साथ ही, इस अनुच्छेद में यह भी उल्लेख किया गया है कि अंग्रेजी को सरकारी प्रयोजनों के लिए जारी रखा जाएगा, परंतु सीमित अवधि के लिए रखा जाएगा।
हालाँकि, शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐसी ही प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया और इसका कारण यह माना जा सकता है कि इसे राज्य विधानसभाओं और शिक्षाविदों की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ दिया गया।
उन्होंने आगे बताया कि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा कई कदम उठाए गए थे, जो इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि वे क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन (इनरिचमेंट) के प्रति आश्वस्त थे और उन्होंने यह कल्पना की थी कि क्षेत्रीय भाषाएं शिक्षा में शिक्षण का उपयुक्त साधन बनेंगी। निर्णय में उल्लिखित कुछ कदम इस प्रकार हैं:
- सभी सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने का आग्रह,
- क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता,
- आठवीं अनुसूची से अंग्रेजी भाषा को हटाना,
- अनुच्छेद 351 की उपस्थिति ने हिंदी भाषा के विकास को निर्देशित किया।
प्रविष्टि 66 की व्याख्या इस प्रकार की जानी है कि सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षण माध्यम का स्थान क्षेत्रीय भाषाएं ले लेंगी और ऐसी स्थिति में समन्वय के लिए मानक तय करने वाले कानून को शिक्षण माध्यम पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय ने तर्क दिया था कि यदि अन्य विश्वविद्यालय गुजरात विश्वविद्यालय की कार्रवाई से प्रभावित हुए और अंग्रेजी, जो शिक्षा का स्वीकृत माध्यम रहा है, के स्थान पर कोई क्षेत्रीय भाषा लागू करने लगे, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि याचिकाकर्ता की दलीलें स्वीकार कर ली जाती हैं तो ऐसी स्थिति में संसद शक्तिहीन हो जाएगी। इस व्याख्या के परिणामस्वरूप “समन्वय” का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा। यही तर्क, एक अलग तरीके से, प्रतिवादी द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था। उनका आशय यह था कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में समाप्त करने वाला राज्य कानून, “समन्वय” वाक्यांश के अंतर्गत प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आता है। न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने इस तर्क को तथ्यात्मक या कानूनी आधार से रहित घोषित कर दिया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने शिक्षा के माध्यम का विषय राज्य विधानमंडलों को सौंपा था क्योंकि वे इसे बेहतर विकल्प मानते थे।
इसका उद्देश्य अंग्रेजी भाषा के स्थान पर किसी क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में स्थापित करना था। इसके लिए, अन्य सभी राज्य धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे, जबकि केवल गुजरात विधानमंडल ने जल्दबाजी में प्रक्रिया अपनाई और गुजराती भाषा को शिक्षा का एकमात्र और विशिष्ट माध्यम प्रस्तावित किया। न्यायाधीश ने सभी राज्यों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को त्यागने की संभावना का सामना करने के लिए “समन्वय” शब्द का विस्तार करने के बजाय “शिक्षा” के प्राकृतिक अर्थ के साथ जाना पसंद किया। इसके अलावा, उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में जारी रखने से मानकों का पतन होगा और अकल्पनीय सहयोग होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी शिक्षा प्रदान करने का साधन बन सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी प्रयास और खर्च करना होगा। उन्होंने मानकों को बनाए रखने के लिए राज्य विधानसभाओं पर भरोसा किया।
आगे कहा गया कि यदि राज्य विधानमंडल अपनी मर्जी से कार्य कर सकता है और विश्वविद्यालयों के हितों के विरुद्ध जा सकता है, तो संसद भी ऐसा ही कर सकती है। यह विश्वास किया जाना चाहिए कि जनता द्वारा निर्वाचित विधायी निकाय के रूप में ये निकाय बुद्धिमत्तापूर्वक तथा जनहित के लिए कार्य करेंगे। इस कारण से, न्यायालय को अप्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करनी चाहिए।
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने अंततः माना कि शिक्षण का माध्यम सूची II की प्रविष्टि 11 के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि राज्य विधानमंडल को किसी विश्वविद्यालय को शिक्षण के विशेष माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा लागू करने के लिए सशक्त बनाने हेतु कानून बनाने का अधिकार है।
गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 के तहत शिक्षा का एक विशेष माध्यम निर्धारित करने की शक्ति
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने अधिनियम की योजना का विश्लेषण किया। गुजरात विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय तथा शिक्षण एवं सम्बद्धता प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय है। तीन संस्थाएं हैं, अर्थात् सीनेट, सिंडिकेट (विधायी निकाय) और शैक्षणिक परिषद (कार्यकारी), जो आवश्यक गतिविधियां संचालित करती हैं और विभिन्न शक्तियां भी रखती हैं। न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 4 के संबंधित खंडों पर भी विचार किया।
उन्होंने कहा कि, जब कोई अधिनियम किसी निगम को उसके द्वारा निर्मित शक्तियां प्रदान करता है, तो वह उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक कार्य करने की शक्ति भी प्रदान करता है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय के पास शिक्षा का विशिष्ट माध्यम लागू करने की शक्ति है। विश्वविद्यालय अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षा का निर्णय करता है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उसके पास शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने की शक्ति होगी। यदि विश्वविद्यालय शिक्षण के अनेक माध्यम निर्धारित कर सकता है, तो वह अधिक उपयुक्त माध्यम को भी विशिष्ट माध्यम के रूप में निर्धारित कर सकता है।
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने टिप्पणी की कि, यदि बम्बई में लागू पिछले कानून और भारत के अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित तुलनीय क़ानूनों पर विचार किया जाए, तो यह देखा जाएगा कि विश्वविद्यालयों ने समान शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में निर्धारित किया था। यदि विश्वविद्यालयों को माध्यम निर्धारित करने की यह मूल शक्ति नहीं दी गई तो इससे उनकी स्वायत्तता प्रभावित होगी तथा अधिनियम के तहत उन्हें प्रदत्त अधिकार भी प्रभावित होंगे। यदि विश्वविद्यालय को ऐसी शक्ति नहीं सौंपी गई तो उसके अधीन सभी सम्बद्ध महाविद्यालय माध्यम के रूप में अलग-अलग भाषाओं को अपना लेंगे और फिर किस भाषा में परीक्षा आयोजित की जाए जैसे मुद्दे उठेंगे। हालाँकि, विश्वविद्यालय को इस शक्ति का प्रयोग तर्कसंगत तरीके से करना चाहिए।

उन्होंने बताया कि धारा 4 का खंड (27) स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय को शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग प्रावधान की शर्तों के अनुसार होना चाहिए। इस खण्ड के क्रियाशील और मूल भाग में विभिन्न अनुच्छेदों के प्रयोग को सामने लाकर इसे स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस तर्क को न्यायाधीश ने खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा कि शिक्षण और परीक्षा के माध्यम को निर्धारित करने की शक्ति धारा 4 के खंड (1) के तहत पहले से ही प्रदान की गई है और खंड (27) शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषाओं के विकास को बढ़ावा देने और उनके उपयोग को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है।
खंड (27) में “निर्देश” के साथ-साथ “परीक्षा” का भी उल्लेख है। यदि यह माना जाता है कि शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने की शक्ति केवल इसी खंड द्वारा प्रदान की गई है, तो इसका अर्थ यह होगा कि परीक्षा के लिए शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने की शक्ति भी इसी खंड द्वारा प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में परिणाम यह होगा कि विश्वविद्यालय के पास गुजराती और हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में परीक्षा आयोजित करने की क्षमता नहीं होगी। दूसरी ओर, यदि संबद्ध महाविद्यालयों में हिंदी और गुजराती के अलावा किसी अन्य भाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में उपयोग करने की क्षमता है, तो विश्वविद्यालय को अपने चुने हुए माध्यम से परीक्षा आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार, इन पर विचार करते हुए, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि खंड (27) केवल उल्लिखित भाषाओं को बढ़ावा देने के कर्तव्य के साथ एक अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, और खंड, किसी भी तरह से, विश्वविद्यालय की अपनी चुनी हुई शिक्षा के माध्यम को निर्धारित करने की शक्ति को प्रभावित करने के लिए नहीं है।
परंतुक के संबंध में न्यायाधीश ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम बनी रहेगी, लेकिन एकमात्र माध्यम के रूप में नहीं। विश्वविद्यालय को शिक्षण के माध्यम के रूप में उल्लिखित भाषाओं में से एक या दोनों को लागू करना है।
परिचालनात्मक और मूल भाग में निश्चित और अनिश्चित उपपदों के प्रयोग के पीछे के तर्क को स्वीकार करते हुए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालय उक्त क्षेत्रीय भाषाओं को अतिरिक्त माध्यम के रूप में निर्धारित कर सकता है, यह तथ्य अनिश्चित उपपदों के प्रयोग से स्पष्ट है; और यह तथ्य कि अंग्रेजी भाषा के बाद निश्चित उपपद आता है, यह दर्शाता है कि इसका प्रयोग एकमात्र माध्यम के रूप में किया जा रहा था। इसके अलावा, इस प्रावधान में यह भी निहित है कि विश्वविद्यालय को समाप्ति की उल्लिखित अवधि के बाद भी अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में जारी रखने का अधिकार है। विश्वविद्यालय को एक निश्चित अवधि के लिए अंग्रेजी को एकमात्र माध्यम बनाने का अधिकार देने वाले प्रावधान को यह जानते हुए अधिनियमित किया गया माना जाता है कि विश्वविद्यालय के पास अंग्रेजी को माध्यम के रूप में निर्धारित करने की शक्ति थी।
न्यायाधीश द्वारा दी गई व्याख्या के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:
- शिक्षण का कोई माध्यम निर्धारित करना;
- हिंदी और गुजराती को बढ़ावा देना;
- हिंदी और गुजराती का प्रयोग शुरू करना;
- उल्लिखित अवधि के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनाये रखना; तथा
- उल्लिखित अवधि पूरी होने के बाद हिंदी और गुजराती के साथ अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा को शिक्षण का माध्यम निर्धारित करना।
असहमति जताने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव द्वारा अंतिम निष्कर्ष
न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला-
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के लिए अनेक माध्यम या एक विशेष शिक्षण माध्यम निर्धारित करने का अधिकार है;
- खंड (27) अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है और अन्य प्रावधानों से प्राप्त निहित शक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है;
- भारत का संविधान विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की देखभाल के लिए राज्य विधानसभाओं और विश्वविद्यालयों पर निर्भर करता है और बदले में विधानसभा ने विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के उत्थान के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपी हैं;
- विश्वविद्यालय को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को किस गति से शुरू किया जाए;
- चूंकि विश्वविद्यालय को शिक्षण का एक विशिष्ट माध्यम निर्धारित करने की शक्ति है, इसलिए अधिनियम की धारा 38A वैध है;
- विश्वविद्यालय अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी और गुजराती को शिक्षण माध्यम के रूप में स्वीकार करते समय अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य नहीं कर रहा था; तथा
- उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया तथा अपील स्वीकार कर ली गयी।
मामले का विश्लेषण
इस मामले ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य और विश्वविद्यालयों को सौंपी गई शक्ति की सीमा को उजागर किया। यद्यपि मूलतः यह देखा गया है कि गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 विश्वविद्यालय को शिक्षण और शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करने का अधिकार देता है, लेकिन यह कोई निरपेक्ष और अप्रतिबंधित शक्ति नहीं है। यदि ऐसी छूट दी गई तो इस बात की संभावना रहेगी कि विभिन्न विश्वविद्यालय अलग-अलग माध्यम अपनाएं, जिससे पूरे देश में शिक्षा में एकरूपता नहीं रहेगी। इसी कारण से, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 4 और 18 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों के उपयोग पर बारीकी से विचार किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि विश्वविद्यालयों को अपने द्वारा स्थापित महाविद्यालयों तथा अपने द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रयुक्त शिक्षा, अध्यापन और माध्यम की देखभाल करने का अधिकार है, किन्तु माध्यम निर्धारित करने की शक्ति इस प्रकार प्रतिबंधित है कि वह कोई विशिष्ट माध्यम निर्धारित नहीं कर सकता। गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 की धारा 4 और धारा 18 के तहत विभिन्न खंडों का उल्लेख करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विश्वविद्यालय की शक्ति एक अतिरिक्त माध्यम निर्धारित करने की है, जो क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसी क्षेत्रीय भाषा को एकमात्र माध्यम नहीं बनाया जा सकता है।
इसके बाद, न्यायालय ने शिक्षा के संबंध में भारत के संविधान में उल्लिखित अतिव्यापी प्रविष्टियों की व्याख्या की है। इस मामले में इस बात पर बहस हुई कि क्या शिक्षा और उससे संबंधित शिक्षण और परीक्षा के माध्यम राज्य या संघ विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विचाराधीन दो प्रविष्टियाँ सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची II की प्रविष्टि 11 थीं। विभिन्न व्याख्याओं पर चर्चा की गई तथा पक्षों द्वारा प्रस्तुत व्याख्याओं पर भी विचार किया गया, जिनमें से कुछ व्याख्याएं असंगत परिणाम लेकर आईं। इसलिए, न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण के साथ आगे बढ़ना उचित समझा ताकि सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त किया जा सके जो देश में शिक्षा के मानकों की दिशा में काम करेगा। इसके बाद, एक स्पष्ट सीमांकन किया गया, अर्थात राज्य विधानमंडल को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र सौंपे गए तथा संघ विधानमंडल को उच्च शिक्षा के क्षेत्र सौंपे गए। इसके अलावा, कहा गया कि जब प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आने वाले मामलों की बात आती है तो संघ को राज्य पर अधिभावी शक्ति का प्रयोग करना होगा, अर्थात, संस्थानों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों को पूरा किया जा रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि करने में संघ को ऊपरी हाथ होगा। इस संबंध में, “शिक्षण के माध्यम” के प्रकाश में सूची I की प्रविष्टि 66 को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह समझा गया कि जब शिक्षण का माध्यम शिक्षा के मानक को प्रभावित करता है, तो यह स्वचालित रूप से सूची I की प्रविष्टि 66 के दायरे में आ जाएगा।
इस मामले में पीठ द्वारा दिया गया निर्णय 5:1 के अनुपात में था। बहुमत ने इस बात का समर्थन किया कि हिंदी या गुजराती को एकमात्र माध्यम नहीं बनाया जा सकता। यह स्वीकार किया गया कि विश्वविद्यालय किसी भी भाषा को माध्यम के रूप में निर्धारित कर सकता है, लेकिन वह एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में होगा; ऐसी भाषा को अनुदेशन और शिक्षा का एकमात्र और अनन्य माध्यम नहीं बनाया जा सकता।
यदि हम असहमतिपूर्ण मत पर गौर करें तो हम पाते हैं कि न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव का मानना था कि शिक्षण का माध्यम शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है और यह एक अविभाज्य तत्व है। इसलिए, जब एक विषय के रूप में “शिक्षा” को राज्य विधानमंडल को सौंपा जाता है, तो शिक्षा का माध्यम उसी से जुड़ा रहता है। राज्य के पास शिक्षा से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है और मानकों में सुधार के मामले में संसद हस्तक्षेप करती है। उन्होंने संवैधानिक ढांचे का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संविधान की योजना भी शिक्षा में शिक्षण माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने का समर्थन करती है।
उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों की आगे व्याख्या की और कहा कि विश्वविद्यालय के पास विशिष्ट माध्यम निर्धारित करने की शक्ति है और इस प्रकार, उनकी राय में, उच्च न्यायालय के आदेश को नकार दिया जाना चाहिए, तथा कहा कि विश्वविद्यालय को शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर उक्त क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने का पूरा अधिकार है।

निष्कर्ष
गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर एवं अन्य (1963) मामले में उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों के आलोक में व्याख्या के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से, सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत का सहारा शिक्षा के क्षेत्र में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच शक्ति के दायरे को अलग करने में लिया गया।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षण और परीक्षा के माध्यम के रूप में किसी भाषा को लागू करने के प्राधिकार के संबंध में अनिश्चितता पर विचार किया गया और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।। अंतर्संबंधित मामलों में राज्य विधानमंडलों पर संघ की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। यदि राज्य विधानमंडल शिक्षा के विषय में कोई कानून बनाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह कानून संघ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उल्लिखित किसी मामले में हस्तक्षेप न करे।
यह मामला भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लिखित प्रविष्टियों के विषय के संबंध में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है तथा पूरे देश में शैक्षिक मानकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
किस राज्य विधानमंडल ने गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 पारित किया?
यह अधिनियम बम्बई राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था।
1949 का अधिनियम कहां लागू था?
यह अधिनियम बम्बई प्रांत में लागू था।
गुजरात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1949 क्यों लागू किया गया?
यह अधिनियम शिक्षण हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने तथा अन्य महाविद्यालयों को संबद्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह बम्बई प्रांत में विश्वविद्यालय शिक्षा को विकेन्द्रीकृत और पुनर्गठित करने के लिए किया गया था।
संदर्भ







