यह लेख Jidnya Thakur जो लॉसीखो से यूएस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड पैरालीगल स्ट्डीज में डिप्लोमा कर रही है, द्वारा लिखा गया है। इस लेख में भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत बिना स्वतंत्र सहमति के करार की शून्यता के बारे में चर्चा की गई है। इसमें वैध, शून्य और शून्यकरणीय (वॉयडेबल) अनुबंध के बीच अंतर के बारे में भी बताया गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
कानूनी रूप से बाध्यकारी करार में प्रवेश करते समय, कानून मांग करता है कि सभी भाग लेने वाले पक्ष अपनी सहमति स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से प्रदान करें। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि सहमति अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त नहीं की जाती है। यदि सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी गई है, तो करार को शून्यकरणीय माना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है या पलटा जा सकता है।
अनुबंध कानून में स्वतंत्र सहमति की अवधारणा व्यक्तियों को उन करारों का फायदा उठाने या उन पर दबाव डालने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें वे वास्तव में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। सहमति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि सभी पक्षों को करार के नियमों और शर्तों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। किसी भी अस्पष्टता या स्पष्टता की कमी से गलतफहमी और संभावित विवाद हो सकते हैं।
स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करने के लिए, कानून की आवश्यकता है कि किसी करार पर बातचीत और हस्ताक्षर के दौरान कोई अनुचित प्रभाव या प्रपीड़न मौजूद न हो। अनुचित प्रभाव तब होता है जब एक पक्ष का दूसरे पर प्रभुत्व होता है और वह उस शक्ति का उपयोग उन शर्तों पर सहमत होने के लिए हेरफेर करने या दबाव डालने के लिए करता है जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। दूसरी ओर, ज़बरदस्ती में किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध करार करने के लिए मजबूर करने के लिए धमकियों या डराने-धमकाने का उपयोग शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, गलत बयानी और धोखाधड़ी भी सहमति को अमान्य कर सकती है। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को किसी करार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान करता है, तो उस सहमति को स्वतंत्र रूप से दी गई सहमति नहीं माना जाता है। गलत बयानी या तो जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है, लेकिन करार को शून्यकरणीय करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण होना चाहिए।
उद्देश्य
करार में शामिल पक्षों को गठित और निष्पादित किए जाने वाले करार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और सहमति और ज्ञान के साथ स्वेच्छा से शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को त्यागा या करार के किसी भी पहलू को स्वतंत्र सहमति के बिना निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए।
स्वतंत्र सहमति से करार
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 13 के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होते हैं, तो इसे वैध सहमति कहा जाता है।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 14 के अनुसार, सहमति के वैध होने के लिए, यह प्रपीड़न, धोखाधड़ी, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव और गलती के बिना होनी चाहिए।
सहमति के बिना करार
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 के अनुसार, जब किसी करार के लिए सहमति प्रपीड़न, धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण होती है, तो उस पक्ष जिसकी सहमति इस प्रकार प्रेरित की गई थी, के विकल्प पर करार शून्यकरणीय हो जाता है ।
इसके अलावा, अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसे करार को रद्द करने या कुछ शर्तों के साथ अनुबंध को लागू करने के लिए प्रेरित किया गया था।
धारा का अपवाद यह है कि यह तीसरे पक्ष के अधिकारों को बचाता है। यदि उन्होंने अनुबंध से संबंधित कुछ खरीदा है जो अनुबंध की शून्यता के कारण रद्द कर दिया गया है, तो तीसरे पक्ष को इससे कोई नुकसान नहीं होगा।
स्वतंत्र सहमति को निरस्त करने वाले तत्व
प्रपीड़न
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15: प्रपीड़न किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना और धमकी देना है। यह किसी व्यक्ति के मन में भय पैदा करके किसी बात पर अपनी बात मनवाने की संभावना रखता है। प्रपीड़न में आया व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगता है जैसे स्वेच्छा से कर रहा हो। प्रपीड़न से किए जाने वाले अनुबंध को रद्द किया जा सकता है।
अनुचित प्रभाव
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16: अनुचित प्रभाव तब होता है जब एक व्यक्ति ऐसे पद पर होता है और दूसरे व्यक्ति का फायदा उठाकर उनसे कुछ ऐसी बातें मनवा लेता है जिन पर वे स्वेच्छा से सहमत नहीं होते। यह अधिकतर तब होता है जब कोई दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो या उस पर प्रपीड़न बना रहा हो; ऐसा अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
धोखाधड़ी
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 17: धोखाधड़ी का मूल रूप से मतलब अनुबंध में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना है। ऐसी धोखाधड़ी करने के लिए, धोखाधड़ी करने वाले पक्ष को इससे कुछ लाभ हो सकता है या जानबूझकर किसी के प्रति गलत बयान दिया जा सकता है। जिसमें जानबूझकर किसी को धोखा देने के लिए झूठ बोलने वाले बयान और झूठे वादे शामिल हैं। अत: अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
गलत बयानी
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18: गलत बयानी एक ऐसी चीज़ है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है, न कि जानबूझकर धोखाधड़ी के रूप में बल्कि ग़लती से, झूठी और गलत जानकारी देकर या अनुबंध के महत्वपूर्ण पहलुओं को छिपाकर।
गलती
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20, 21, और 22: दोनों पक्षों या एक पक्ष के लिए इस तरह से अज्ञात विश्वास या धारणा रखना गलती है। यदि अनुबंध इस प्रकार बनाया गया है, तो इसे इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि पक्षों को तथ्यों की जानकारी नहीं थी या वे तथ्यों से अनजान थे।
वैध, शून्य और शून्यकरणीय अनुबंधों के बीच अंतर
वैध अनुबंध
एक वैध अनुबंध में वैध माने जाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। इनमें पक्षों की स्वतंत्र सहमति शामिल है; अनुबंध के पक्षों को अनुबंध करने में सक्षम होना चाहिए, वैध उद्देश्य और वैध प्रतिफल होना चाहिए; और इसे स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- स्वतंत्र सहमति: अनुबंध के तहत किसी बात पर सहमत होने वाले पक्षों को बिना किसी धोखाधड़ी, गलत बयानी, प्रपीड़न , अनुचित प्रभाव या गलती के अनुबंध पर सहमत होना चाहिए। इसलिए पक्षों ने स्वतंत्र सहमति दी है।
- अनुबंध के लिए सक्षम: पक्षों की योग्यता आवश्यक है, जैसे कि उम्र, स्वस्थ दिमाग के मामले में कानूनी रूप से सक्षम होना, और कानून द्वारा अयोग्य नहीं होना।
- वैध प्रतिफल और उद्देश्य: करार कुछ मूल्य का होना चाहिए न कि उपहार का। यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध या अवैध प्रकृति का भी नहीं होना चाहिए।
- स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए: करार को पहले से ही कानून द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए या करार का अवैध रूप नहीं माना जाना चाहिए।
शून्य अनुबंध
शून्य अनुबंध वे अनुबंध हैं जो शुरू से ही शून्य हैं, जिनका कोई वैध उद्देश्य नहीं है, अनुबंध के लिए सक्षम नहीं हैं, स्वतंत्र सहमति के बिना लागू करने योग्य नहीं हैं, और जिनमें अस्पष्ट नियम और शर्तें शामिल हैं।
- प्रारंभ से ही शून्य: जो अनुबंध प्रारंभ से ही शून्य हैं, वे कानूनी रूप से बाध्यकारी और स्वीकार्य नहीं हैं। इसमें वे अनुबंध शामिल हैं जिन्हें उनके गठन के प्रारंभिक चरण से निष्पादित करना असंभव है। इसलिए, यह कहा जाता है कि अनुबंध शुरू से ही शून्य है।
- अनुबंध के लिए सक्षम नहीं: यदि पक्ष अनुबंध के लिए सक्षम नहीं हैं, तो अनुबंध को शून्य कहा जाता है, जैसे कि 18 वर्ष से कम आयु के विकृत दिमाग वाले या कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के मामले में।
- वैध उद्देश्य न होना: कानून और व्यवस्था की अवज्ञा करने या कानून के विरुद्ध होने के लिए किया गया अनुबंध। अत: ऐसा अनुबंध शून्य है।
- स्वतंत्र सहमति के बिना: प्रपीड़न , अनुचित प्रभाव, गलत बयानी, धोखाधड़ी या गलती के तहत किया गया अनुबंध शून्य है।
- अस्पष्ट नियम और शर्तें: ऐसे तरीके से या ऐसे मानदंडों के साथ बनाए गए अनुबंध जो अस्पष्ट हैं, समझे नहीं जा सकते हैं, या किसी की राय में गलतियाँ पैदा कर सकते हैं, शून्य हैं।
शून्यकरणीय अनुबंध
शून्यकरणीय अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो एक पक्ष के विकल्प पर मान्य होता है और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है; इस प्रकार, ऐसा अनुबंध प्रकृति में शून्यकरणीय है। जिन परिस्थितियों में अनुबंध शून्यकरणीय है उनमें स्वतंत्र सहमति की कमी, अनुबंध का उद्देश्य वैध नहीं होना, पक्षों का अनुबंध करने में सक्षम नहीं होना, ऐसे अनुबंध को रद्द करने का अधिकार और अनुबंध को तत्काल खत्म न करना शामिल है।
- स्वतंत्र सहमति का अभाव: सहमति के स्वतंत्र होने के लिए, सबसे पहले इसे प्रपीड़न , अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी और गलती से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा, सहमति की कमी एक करार बनाने में सक्षम नहीं है, और ऐसे अनुबंध शून्यकरणीय हैं।
- अनुबंध का उद्देश्य वैध नहीं होना: अनुबंध का उद्देश्य वैध नहीं होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता है और इसे शून्यकरणीय घोषित नहीं किया जा सकता है।
- पक्षों का अनुबंध करने में सक्षम नहीं होना: अवयस्क पक्ष अनुबंध नहीं कर सकते हैं, और यदि ऐसा अनुबंध बनता है, तो यह प्रकृति में शून्य है और साथ ही अयोग्य या दिवालिया के साथ उन पक्षों के विकल्प पर शून्यकरणीय है जो अनुबंध करने में अक्षम हैं।
- किसी अनुबंध को रद्द करने का अधिकार: एक शून्यकरणीय अनुबंध में, उन पक्षों को अधिमान्य (प्रेफरेंशियल) अधिकार होता है जिनके पास स्वतंत्र सहमति की कमी है या अनुबंध के लिए अक्षम हैं और उद्देश्य वैध नहीं है। इसलिए, यदि यह बात ऐसे किसी पक्ष को पता चलती है, तो वे अनुबंध रद्द कर सकते हैं।
- अनुबंध को तत्काल खत्म नहीं किया जा सकता: अनुबंध को तत्काल बंद नहीं किया जा सकता। अनुबंध तब तक कार्यान्वित होता है जब तक पक्षों द्वारा अनुबंध को वैध बनाने की संभावना नहीं हो जाती।
परिणाम एवं उपाय
- निरस्तीकरण (रिसेशन) (आईसीए, 1872 की धारा 19): अनुचित प्रभाव, प्रपीड़न , गलत बयानी या धोखाधड़ी के तहत पक्ष द्वारा अनुबंध को रद्द करना निरस्तीकरण है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 के तहत अनुबंध रद्द करने का ऐसा अधिकार है।
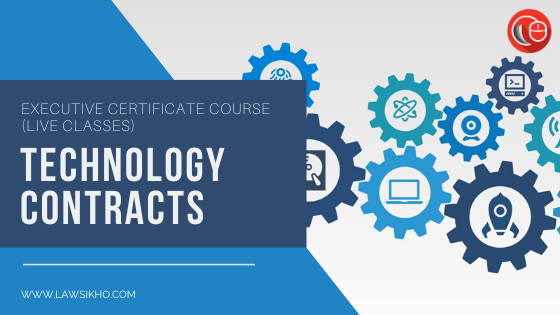
- हर्जाना (आईसीए, 1872 की धारा 19 और धारा 73): भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 19 के तहत यह दिया गया है कि पक्ष ऐसे शून्यकरणीय अनुबंध में हुए नुकसान के लिए दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 अनुबंध के उल्लंघन के लिए मुआवजे को शामिल करती है।
- पुनर्स्थापन (रेस्टीट्यूशन) (आईसीए, 1872 की धारा 64): भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 64 के तहत यह दिया गया है कि जब कोई अनुबंध निरस्तीकरण के समय शून्यकरणीय हो जाता है, तो शून्यकरणीय अनुबंध ने अनुचितता से बचने के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्राप्त कोई भी लाभ वापस कर दिया जाना चाहिए।
- सुधारना (विनिर्दिष्ट अनुतोष (स्पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम, 1963 की धारा 31– धारा 34): यह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 और धारा 34 की व्याख्या करता है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी अनुबंध के नियमों या शर्तों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा अनुबंध शून्यकरणीय हो जाता है, तो यह धारा अनुबंध को बचाती है और ऐसी शर्तों को तदनुसार सुधारने का अधिकार देती है।
मामले का अध्ययन
सत्य ब्रता घोष बनाम मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी (1954)
मामले के तथ्य
- इस मामले में मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी ने भूमि के टुकड़े को इस रूप में प्रस्तुत किया कि उस पर कोई मांग नहीं थी।
- सत्य ब्रता घोष ने मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया।
- इसलिए, सत्या ब्रता जमीन खरीदने के लिए सहमत हो गए।
- करार में प्रवेश करने के बाद, घोष को पता चला कि संपत्ति मांग के अधीन थी।
- हालाँकि, मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी द्वारा इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था।
न्यायालय का निर्णय
- इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी ने सत्य ब्रता घोष को संपत्ति की स्थिति के बारे में गलत बयानी दी थी।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी ने तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था और अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुबंध शून्यकरणीय था।
- सत्य ब्रता घोष भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के तहत गलत बयानी के कारण अनुबंध को रद्द करने के हकदार थे।
डेरी बनाम पीक
मामले के तथ्य
- इस मामले में एक कंपनी थी जिसे ट्राम कंपनी के नाम से जाना जाता था।
- ये कंपनियाँ चाहती थीं कि लोग उनकी कंपनियों के शेयरों में निवेश करें।
- इसके अलावा, उन्होंने एक विवरण-पत्रिका (प्रॉस्पेक्टस) जारी किया कि उन्हें भाप से चलने वाली ट्रामों जो घोड़े से चलने वाली ट्रामों की तुलना में अधिक कुशल थीं का उपयोग करने की अनुमति है।
- प्रमुख कारक यह था कि उन्हें सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता थी।
- सरकार ने मंजूरी रद्द कर दी थी।
- इस प्रकार, पीक ने कंपनी के शेयरों में निवेश किया।
- जब कंपनी को कोई मंजूरी नहीं मिली, तो मूल्य गिर गया और पीक ने अपना पैसा खो दिया।
- इसलिए, पीक ने कंपनी के निदेशकों पर मुकदमा दायर किया।
निर्णय
- हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि धोखाधड़ी के ऐसे दावे पर विचार करने के लिए पीक को इसे साबित करने की जरूरत है।
- इसलिए, शेयरधारकों द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि कंपनी के निदेशक बेईमान थे।
- निदेशकों का विश्वास था कि कंपनी को मंजूरी मिल सकती है; इसलिए, कंपनी के लापरवाह होने के बावजूद, इसका पूरी तरह से यह मतलब नहीं है कि वे झूठ बोल रहे थे।
चिक्कम अम्मीराजू बनाम चिक्कम सेशम्मा
मामले के तथ्य
- इस मामले में चिक्कम अम्मीराजू और उनका परिवार संपत्ति विवाद में शामिल थे।
- चिक्कम अम्मीराजू की पत्नी शेषम्मा और बेटे सुब्बम्मा को चिक्कम अम्मीराजू के पक्ष में संपत्ति से अपना अधिकार मुक्त करने के लिए कहा गया।
- अम्मीराजू ने बात न मानने पर आत्महत्या करने की धमकी दी।
- उसके जीवन के डर से, शेषम्मा और सुब्बम्मा ने रिहाई विलेख (डीड) निष्पादित किया।
- और चिक्कम अम्मीराजू की मांग के अनुसार अधिकार हस्तांतरित कर दिए थे।
- शेषम्मा और सुब्बम्मा ने यह तर्क देकर विलेख की वैधता को चुनौती दी कि विलेख के लिए उनकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी और इसे प्रपीड़न प्राप्त की गई थी। उन्होंने इसे एक शून्यकरणीय विलेख माना।
निर्णय
- मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि चिक्कम अम्मीराजू द्वारा आत्महत्या की धमकी भारतीय न्याय संहिता द्वारा निषिद्ध है और यह भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रपीड़न भी है।
- अदालत ने पाया कि करार ज़बरदस्ती किया गया था और शून्यकरणीय था।
- अदालत ने फैसला सुनाया कि रिहाई विलेख शेषम्मा और सुब्बम्मा के विकल्प पर शून्यकरणीय थी। इसका मतलब है कि उन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के तहत करार को रद्द करने का अधिकार था।
लाडली प्रसाद जयसवाल बनाम करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड (1963)
मामले के तथ्य
- इस मामले में लाडली प्रसाद जयसवाल करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध एजेंट थे।
- कंपनी के निर्णयों में प्रबंध एजेंट का प्रभाव होता है।
- कंपनी और जयसवाल के बीच करार पर हस्ताक्षर किये गये।
- कंपनी में जयसवाल की प्रभावशाली स्थिति के कारण करार पर पहले ही अनुचित प्रभाव में हस्ताक्षर किए गए थे।
- कंपनी के अन्य शेयरधारकों और पक्षों ने दावा किया है कि कंपनी पर प्रपीड़न डालकर करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।
निर्णय
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह करार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 16 के तहत अनुचित प्रभाव के अंतर्गत आता है।
- अनुचित प्रभाव वो है जहां कोई व्यक्ति दूसरों की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के तहत अनुबंध शून्य कर इसे रद्द करने का अधिकार दिया था।

निष्कर्ष
अनुबंध कानून में कहा गया है कि अनुबंध स्वतंत्र सहमति का होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति के विरुद्ध किए गए अनुबंध स्वभावतः शून्यकरणीय होते हैं। इस प्रकार, ऐसे अनुबंधों में प्रपीड़न , अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी और गलती से बने अनुबंध शामिल हैं।
संदर्भ







