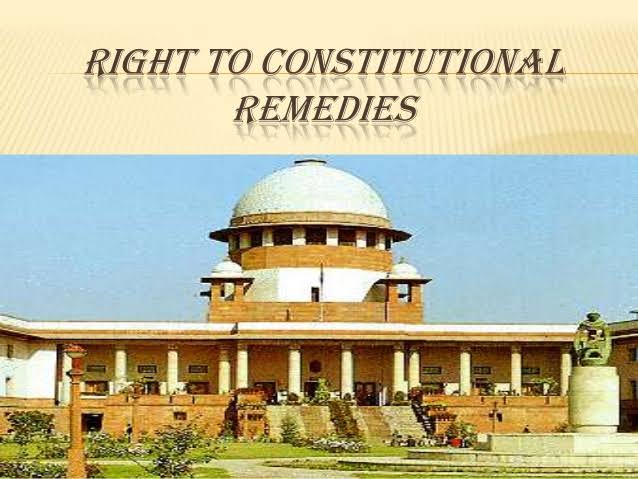यह लेख Titas Biswas द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान के महत्व, इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों और उनके उल्लंघन के उपायों पर चर्चा की है। उन्होंने भारतीय संविधान में रिट, इसके प्रकार और संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा की है तथा भारतीय कानूनी प्रणाली में इसके योगदान का पता लगाया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से गैर-नागरिकों को उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उपचार के मार्ग पर मार्गदर्शन भी करता है, जो गैर-नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक अधिकारों से तात्पर्य भारतीय संविधान के भाग III में उल्लिखित अधिकारों से है, जिसमें ‘मौलिक अधिकारों’ का प्रावधान है। कानूनी कहावत “यूबी जस इबी रेमेडियम” इस पहलू पर सटीक बैठती है, जो यह उपदेश देती है कि जहां अधिकार है, वहां उपाय भी है।
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय कानूनी प्रणाली का आधार इस प्रकार तैयार किया है, जिसमें इन अधिकारों की रक्षा हो। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 को शामिल किया गया है। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अनुसार, यह “संविधान की आत्मा और उसका हृदय है।” भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों को व्यक्ति और उसकी नागरिक स्वतंत्रता को अत्याचारी विधायी या कार्यकारी कार्यों से बचाने के लिए शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालयों को किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिनियम को शून्य घोषित करने का अधिकार है।
भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के आधार के रूप में संवैधानिक उपचार का अधिकार
भारतीय संविधान को हमारे राष्ट्र के आधारभूत मानदंड के रूप में स्वीकार किया गया है, जो अपने प्रावधानों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, तथा भारतीय विधिक प्रणाली के सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक उपचार से हमारा तात्पर्य उन उपचारों से है जो भारतीय संविधान ऐसे मामलों में प्रदान करता है जहां किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। भाग III के तहत प्रदत्त अधिकार भारतीय संविधान के प्रावधानों पर स्पष्ट रूप से अपनी छाप छोड़ते हैं, जिससे यह भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण खंडों में से एक बन जाता है।
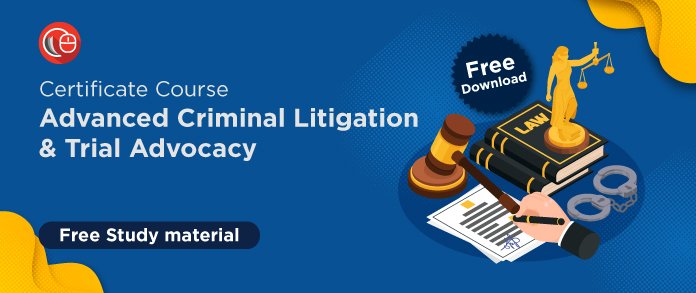
संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का व्यापक विवरण दिया गया है, जिसमें ऐसे अधिकारों को मोटे तौर पर छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी अधिकार के उल्लंघन से बचाने के लिए संवैधानिक उपचार अस्तित्व में आते हैं। जबकि लेख में संवैधानिक उपचारों पर चर्चा की गई है, छह व्यापक रूप से वर्गीकृत मौलिक अधिकारों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। ये हैं-
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30), तथा
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- भारतीय संविधान में भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है।
संविधान का अनुच्छेद 13
भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो कानून भारतीय संविधान में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जो इसके लागू होने से पहले के हैं, वे अस्तित्व में पूरी तरह से शून्य होंगे। अनुच्छेद 132(2) भारतीय संविधान के भाग III के तहत प्रदत्त अधिकारों का हनन करके संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायी क़ानून को लागू करने से रोकता है। ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, उस उल्लंघन की सीमा तक अमान्य माना जाएगा।
संविधान का अनुच्छेद 14
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उन प्रमुख अनुच्छेदों में से एक है जो किसी व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता के बारे में निर्दिष्ट करता है और यह भी कहता है कि भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान का यह प्रावधान किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वह नागरिक हो या न हो, तथा यह देश के भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है।
संविधान का अनुच्छेद 15
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसी व्यक्ति के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यह अनुच्छेद, अपने खंड 2(a) और (b) के अंतर्गत आगे यह प्रावधान करता है कि किसी भी नागरिक को, चाहे उसका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान कुछ भी हो, दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जाएगा या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जिनका प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य द्वारा किया जाता है के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा।
संविधान का अनुच्छेद 16
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर उसके विरुद्ध भेदभाव पर प्रतिषेध करता है। आगे विस्तार से कहें तो, अनुच्छेद 16 ने राज्य प्राधिकार को पिछड़े वर्गों के लोगों जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है के लिए विशेष प्रावधान बनाए रखने और बनाने का अधिकार दिया है।
संविधान के अनुच्छेद 17 और 18
जहां भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले किसी भी कार्य की निंदा करता है, उसे आपराधिक कार्य मानता है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 18 किसी भी व्यक्ति को उपाधि देने पर प्रतिबन्ध लगाता है।
संविधान का अनुच्छेद 19
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था, विश्वास और राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद कई मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, वे निम्नलिखित हैं:
- स्वतंत्रतापूर्वक एवं शांतिपूर्वक तथा बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार;
- संघ बनाने का अधिकार;
- भारत के क्षेत्र में बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार;
- भारतीय प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार;
- संपत्ति का स्वामित्व, धारण या निपटान करने का अधिकार; और
- अपनी पसंद का कोई भी पेशा अपनाने या कारोबार या व्यापार करने का अधिकार हैं।
अनुच्छेद में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि इन अधिकारों में कुछ प्रतिबंध शामिल हैं तथा ये उचित प्रतिबंधों से संबंधित हैं।
संविधान का अनुच्छेद 20
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उसके किसी ऐसे कार्य के जो कानून का उल्लंघन करता हो। बशर्ते कि ऐसा कानून कथित कार्य के किए जाने के समय लागू होना चाहिए। इसमें आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 20(3) यह भी प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात आत्म-दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अधिकार।
संविधान का अनुच्छेद 21
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का दायरा विभिन्न न्यायिक व्याख्याओं और उनके द्वारा स्थापित कानूनी मिसालों से और अधिक विस्तृत हो गया है। इस कदम ने मनमाने कार्यों तथा किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध जागरूकता का मार्ग प्रशस्त किया है।
संविधान का अनुच्छेद 22
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि उसे अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार द्वारा बचाव पाने तथा न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए बाध्य करता है।
संविधान के अनुच्छेद 23 और 24
अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 23 विशेष रूप से मानव तस्करी और जबरन श्रम में शोषण से संबंधित है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 24 कारखानों में काम करने के उद्देश्य से बाल श्रम पर रोक लगाता है, विशेष रूप से चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों पर रोक लगाता है।
संविधान के अनुच्छेद 25 से 28
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25-28 के माध्यम से धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद कुछ उचित प्रतिबंधों के साथ किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार सुनिश्चित करते हैं। ये प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के साथ-साथ इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं।
इसके अलावा, अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों की स्थापना का प्रावधान करता है तथा उन्हें धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थाओं को बनाए रखने की शक्तियां प्रदान करता है। यह अनुच्छेद धार्मिक संस्थाओं को अपना प्रशासन स्वयं चलाने, अपने मामलों का प्रबंधन करने तथा स्वयं संपत्ति अर्जित करने की भी अनुमति देता है, चाहे वह संपत्ति चल या अचल हो सकती है। यह अनुच्छेद आगे निर्देश देता है कि ऐसी संपत्ति का प्रशासन कानून के अनुसार होना चाहिए।
अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार से संबंधित करों के भुगतान से छूट प्रदान करता है। अंत में, अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में किसी विशेष धर्म के प्रावधान पर प्रतिबंध लगाता है, जो धर्म के मामलों में तटस्थता (न्यूट्रलिटी) सुनिश्चित करता है।
संविधान का अनुच्छेद 29
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भारत के राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले उन नागरिकों की विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के अधिकार की रक्षा करता है, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि है। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।

संविधान का अनुच्छेद 30
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के बारे में व्यापक है तथा इसमें धर्म और भाषा दोनों के आधार पर इसका विस्तार किया गया है। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को स्वयं की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ऐसे संस्थानों का प्रबंधन किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है।
मौलिक अधिकारों की घोषणा उनके प्रवर्तन के उचित उपाय के बिना अप्रभावी है। किसी उपचार का अस्तित्व किसी अधिकार के प्रभावी प्रवर्तन की उपस्थिति तथा उसे मूर्त वास्तविकता में रूपान्तरित करने को सुनिश्चित करता है। उपचार के बिना अधिकार कुछ भी नहीं है। इस पर विचार करते हुए, संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया, जो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय
संविधान का हृदय और आत्मा
अनुच्छेद 32 की उत्पत्ति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई, जब नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बन गया। स्वतंत्रता-पूर्व के समय में, भारतीय कानूनी संदर्भ में एक आधारभूत कानूनी ढांचे की अत्यंत आवश्यकता थी, जो मनमानी और शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से कार्य कर सके। इस विश्वास ने एक क्रांतिकारी विकास को आमंत्रित किया जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से सुरक्षा मिली।
यह अनुच्छेद न केवल एक सैद्धांतिक परिकल्पना के रूप में कार्य करता है, बल्कि भाग III के तहत व्यक्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का आश्वासन भी देता है। जैसा कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने एक बार कहा था, “यदि मुझसे इस संविधान में किसी विशेष अनुच्छेद का नाम बताने के लिए कहा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है – ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान अमान्य हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 32) के अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का उल्लेख नहीं कर सकता है।”यह संविधान की आत्मा और हृदय है।”
सर्वोच्च न्यायालय की अप्रतिबंधित शक्ति
अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (2) के तहत रिट, निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के इस खंड के अंतर्गत रिटों का विविधीकरण (जिस पर बाद में विस्तार से चर्चा की गई है) किया गया है, तथा इसके विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, जो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस), परमादेश (मैंडामस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), अधिकार पृच्छा (क्यो वारंटो) और उत्प्रेषण (सर्टिओरारी)। इस व्यापक शक्ति के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अनुच्छेद 32 एक ऐसा अधिकार है जो अन्य अधिकारों को सुदृढ़ (रेनफोर्स) करता है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(1) के तहत कानूनी रूप से तैयार किया गया है, जो किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए उचित कार्यवाही के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।
इसके अलावा, अनुच्छेद 32(4) में यह प्रावधान है कि जिन अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी दी गई है, यानी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, जब तक कि संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा जाए। हालाँकि, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान भारतीय संविधान के भाग III के तहत निहित अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 19 ऐसे आपातकाल की घोषणा जारी रहने तक निलंबित रहेगा। इसके अलावा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के अनुसार, यदि सशस्त्र विद्रोह के बजाय युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत सूचीबद्ध अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। हालाँकि, अनुच्छेद 359 के आधार पर राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
इन अधिकारों का लाभ कौन उठा सकता है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने मौलिक अधिकार को लागू कर सके। नागरिक और गैर-नागरिक दोनों अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग III के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपचार प्रदान करते हैं।
भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, रोजगार का अधिकार जैसे अधिकार भारत के नागरिकों तक ही सीमित हैं, कानून के समक्ष समानता, तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा जैसे अधिकार किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं, चाहे उसकी नागरिकता की स्थिति कुछ भी हो। इसलिए, इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी विदेशी पर्यटक के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसे व्यक्ति अदालत से अपने अधिकारों की बहाली का दावा कर सकते हैं।
नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के बीच मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति की समावेशिता (इन्क्लूजिवनेस) यह साबित करती है कि इन अधिकारों का लाभ किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है, बशर्ते कुछ अपवाद हों, जो गैर-नागरिकों को इनसे वंचित कर सकते हैं।
आइये अब हम विभिन्न मामलों की महासागरीय गहराई में गोता लगाएँ, जिनकी चर्चा नीचे की गई है।
प्रासंगिक मामले
स्किल लोट्टो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2020)
स्किल लोट्टो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2020) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के भाग III के तहत उल्लिखित अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। इसने आगे कहा कि संविधान का यह विशेष प्रावधान मूल संरचना के अभिन्न तत्वों में से एक है। अदालत ने इस अनुच्छेद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि कानून के शासन को लागू करना आवश्यक है।
रशीद अहमद बनाम म्युनिसिपल बोर्ड, कैराना भारत संघ और राज्य (1950)
रशीद अहमद बनाम द म्युनिसिपल बोर्ड, कैराना भारत संघ और राज्य (1950) का मामला, किसी के खुद का व्यवसाय करने के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित था, जिसे कथित तौर पर कैराना के म्युनिसिपल बोर्ड ने रोक दिया था। नगर निगम बोर्ड ने मनमाने ढंग से कार्य करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन किये गये अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) को बेतुके कारणों के आधार पर खारिज कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को उपनियमों का कथित उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के महत्व को बरकरार रखते हुए कहा कि यह विशेषाधिकार रिट जारी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मौलिक अधिकार को बहाल करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्देश देने या आदेश देने की शक्ति तक भी विस्तारित है।

मोहम्मद मोइन फ़रीदुल्लाह कुरैशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020)
मोहम्मद मोइन फ़रीदुल्ला कुरैशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2020) के मामले में याचिकाकर्ता ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टाडा) के तहत उस पर लगाई गई सजा को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 32 को लागू करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे किशोर होने का लाभ दिया जाना चाहिए, जिसे मामले में पहले भी उजागर किया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि, यद्यपि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त साधन है, लेकिन इसे किसी व्यक्ति के संबंध में सामान्य उपाय के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं दिया गया है, विशेषकर किसी कानूनी निर्णय को चुनौती देने के लिए दिया गया है। इसने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में जहां अदालत द्वारा दी गई सजा अंतिम हो, और उसकी आपराधिक अपील पर मुकदमा चलाया गया हो और उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया हो, वहां सजा को उलटने के लिए अनुच्छेद 32 का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226
संविधान के भाग V में शामिल अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालयों को रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित पाँच प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
- बंदी प्रत्यक्षीकरण,
- परमादेश,
- प्रतिषेध,
- अधिकार-पृच्छा, और
- उत्प्रेषण,
इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो उपाय प्रदान किया गया है, वह केवल मौलिक अधिकारों की सीमा रेखा से आगे तक फैला हुआ है तथा इसमें अन्य कानूनी उद्देश्य भी शामिल हैं, जिनमें प्रशासनिक दुरुपयोग भी शामिल है। जबकि अनुच्छेद 32 का केन्द्रीय स्वरूप मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है।
उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों पर निगरानी रखने की अधीक्षक शक्ति का उल्लेख है। यह प्रावधान प्रभावी तरीके से कानून के शासन और न्याय प्रशासन को बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। उच्च न्यायालय अपनी अधीक्षक शक्ति का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी कर सकते हैं तथा इस बात पर नजर रख सकते हैं कि न्याय का उचित प्रशासन हो रहा है या नहीं। उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है जहां किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227(2) के अनुसार, उच्च न्यायालय किसी भी कानूनी प्रक्रिया या सूत्र की व्यापकता को प्रभावित किए बिना निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त हैं:
- अनुच्छेद 272(2)(a) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय विभिन्न लंबित न्यायिक कार्यवाहियों के रिकॉर्ड, निपटाए गए मामलों की संख्या या कोई भी जानकारी जो न्याय के उचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रासंगिक हो सकती है, मांग सकते हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272(2)(b) में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय की प्रक्रियाओं और संचालन को नियंत्रित करने के लिए नियम और विनियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 272(2)(c) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालयों को अदालती रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेजों, वित्तीय खातों आदि के रखरखाव को विनियमित करने का अधिकार है।
ये पर्यवेक्षी शक्तियां व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उनके लिए उपलब्ध संवैधानिक उपचारों की पूरक हैं। उच्च न्यायालय को ऐसे अधिकार प्रदान करने से अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यकुशलता सुनिश्चित होती है, तथा न्याय के समुचित प्रशासन पर निगरानी रखी जाती है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों में अंतर
| आधार | सर्वोच्च न्यायालय | उच्च न्यायालय |
| अधिकार क्षेत्र का दायरा | सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी भी उच्च न्यायालय से अधिक व्यापक है। इसमें मूल अधिकार क्षेत्र, अपील अधिकार क्षेत्र और सलाहकार अधिकार क्षेत्र शामिल हैं। | किसी विशेष राज्य के उच्च न्यायालयों के पास सीमित मूल अधिकार क्षेत्र, अर्थात् रिट है। वे मूलतः अपने अधीनस्थ राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों से मामलों की अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं। |
| मूल अधिकार क्षेत्र | सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य आरंभिक अधिकार क्षेत्र भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, अथवा एक ओर भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच होता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल दो राज्यों के बीच के विवादों को भी शामिल करता है। | भारत में प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिटों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, तथा उत्प्रेषण के माध्यम से निर्देश या आदेश जारी करने का मूल अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और उनके उल्लंघन से निपटने के लिए इस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। |
| अपीलीय अधिकार क्षेत्र | सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132(1), 133(1) या 134 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
सिविल मामलों में – सिविल मामलों में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति दी जाती है यदि वह प्रमाणित करता है कि: a) ऐसे मामले में कोई सामान्य सारवान विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, (b) उसकी राय में, मामले की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उचित जांच की आवश्यकता है तथा उसका निपटारा उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। आपराधिक मामलों में – किसी उच्च न्यायालय से आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति है यदि ऐसा उच्च न्यायालय – a) दोषमुक्ति के फैसले को पलट देता है और अभियुक्त को मृत्युदंड, या आजीवन कारावास या कम से कम दस वर्ष के कारावास की सजा देता है, और b) अपने अधीनस्थ न्यायालयों में से किसी एक से किसी मामले को अपने विवेक से वापस ले लेता है, ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। हालाँकि, दी जाने वाली सज़ा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस वर्ष या उससे अधिक कारावास की होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत भर के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर विशेष अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी सुरक्षित रखा है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत के प्रादेशिक प्रभाग के भीतर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा जारी किसी भी डिक्री, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। |
भारत के उच्च न्यायालयों का अपीलीय अधिकार क्षेत्र केवल उनके पास ही है। सभी मामले, चाहे वे सिविल हों या आपराधिक, उच्च न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं, ताकि उनका तथ्यात्मक और विधिक ढंग से निपटारा किया जा सके।
सिविल मामलों में – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अनुसार, ऐसे मामलों में अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी जहां विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो। उच्च न्यायालय को किसी भी ऐसे मुद्दे को निपटाने के लिए आवश्यक निर्धारित करने का अधिकार है, जहां ऐसे मुद्दे को निचली अदालत या निचली अपीलीय अदालत (यदि कोई हो) द्वारा संबोधित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों जहां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मुद्दों को गलत तरीके से निर्धारित किया गया था में भी ऐसे मामलों को संबोधित करने का अधिकार है। आपराधिक मामलों में – उच्च न्यायालयों के अपीलीय अधिकार क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि, दोषमुक्ति और अन्य दंडों की अपीलों की समीक्षा और सुनवाई शामिल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374) के अनुसार, सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषसिद्धि के मामले में अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अपनी नियमित अपीलीय शक्ति के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के पास कुछ अंतरिम आदेशों, जैसे जमानत या कार्यवाही पर रोक, की समीक्षा करने की भी शक्ति होती है। |
| सलाहकार अधिकार क्षेत्र | भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकार अधिकार क्षेत्र की विशेष शक्ति प्राप्त है। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपनी सलाहकार शक्तियों पर रखे गए कानूनी और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर राय देने में सक्षम बनाता है।
राष्ट्रपति इस प्रावधान को लागू करके कानूनी मार्गदर्शन चाहते हैं और यद्यपि न्यायालय का ऐसा सुझाव बाध्यकारी नहीं है, फिर भी यह उपयोगी परिणाम लेकर आता है। |
भारत के उच्च न्यायालयों को विशेष रूप से परामर्श अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, लेकिन वे उन मुद्दों पर विचार करने के लिए पात्र हैं जो चिंताजनक हैं और जिनका समाधान आवश्यक है। हालाँकि, उच्च न्यायालयों को आवश्यकता पड़ने पर सरकारी अधिकारियों और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों को कानूनी जटिलताओं के संबंध में मार्गदर्शन देने का अधिकार है। |
| रिट अधिकार क्षेत्र | भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने तथा उनके उल्लंघन से बचाने के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है।
ये रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती हैं जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न्यायालय में आवेदन करता है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। ये रिट हैं; बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार-पृच्छा, और उत्प्रेषण है। |
भारत के उच्च न्यायालयों को रिटों जिनके नाम हैं; बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, तथा उत्प्रेषण के माध्यम से निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 भारत के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है।
उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना, उल्लंघन होने पर मौलिक अधिकारों को बहाल करने तथा अन्य प्रशासनिक या सामान्य कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। |
| न्यायालय की अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति | भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वयं के प्रति की गई अवमानना भी शामिल है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 में परिलक्षित होता है।
भारतीय संविधान के अलावा, न्यायालय की अवमानना और उसके दंड के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 145 के साथ सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियम, 1975 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही को विनियमित करने के नियमों के नियम-2, भाग-I के अंतर्गत उल्लिखित नियमों के अलावा, न्यायालय निम्नलिखित के तहत कार्यवाही शुरू कर सकता है:
|
भारत के उच्च न्यायालयों को विशेष रूप से “ऑन रिकॉर्ड-न्यायालय” के रूप में नामित किया गया है, जो उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है।
यह शक्ति न्यायालय की प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन तथा उसके द्वारा जारी आदेशों के सुचारू रख-रखाव पर नजर रखती है। आगे यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय ऐसे किसी भी आचरण के विरुद्ध कार्रवाई कर सकें जो उनके कामकाज और न्याय के समुचित प्रशासन में बाधा डालता हो। |
रिट क्या हैं?
रिट आदेश या निर्देश होते हैं जो या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। ‘रिट’ शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द ‘गेव्रिट’ से हुई है, जिसका अर्थ है लिखित बात। रिट को एक दूसरे के स्थान पर ‘विशेषाधिकार रिट’ भी कहा जा सकता है। ‘विशेषाधिकार’ शब्द से विशिष्ट अधिकार या विशेषाधिकार का बोध होता है। प्रारंभिक समय में, अंग्रेजी कानून के न्यायशास्त्र के तहत, ‘विशेषाधिकार’ या ‘विशेषाधिकार शक्तियां’ संप्रभुता का प्रतीक थीं, जो विशेष रूप से क्राउन या ऐसे शक्तियों को आगे सौंपने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के पास होती थीं। मुख्यतः, विशेषाधिकार रिट इंग्लैंड में प्रचलित थी, क्योंकि इन्हें तब जारी किया जाता था जब राजा द्वारा लंदन में किंग्स बेंच के तहत शाही डिक्री पारित की जाती थी।
भारतीय न्याय प्रणाली ने विशेषाधिकार रिट की अवधारणा को अधिक व्यावहारिक तरीके से शामिल किया, जिसमें न्यायपालिका अपने न्यायिक उदाहरणों और व्याख्या के माध्यम से प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कार्य करती है। भारत में रिट का उद्भव 1773 के विनियमन अधिनियम से माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बाद में, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर तीन प्रेसीडेंसी शहरों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय स्थापित किये गये, जिन्हें रिट जारी करने का भी अधिकार दिया गया था।
प्रेसिडेंसी उच्च न्यायालयों को उनके विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत परमादेश रिट जारी करने का अधिकार दिया गया, जिसका कानूनी प्रावधान विशिष्ट अनुतोष (रिलीफ) अधिनियम, 1877 की धारा 45 के अंतर्गत किया गया था। जबकि, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 491 के अन्तर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका प्रस्तुत की गई थी। विशेषाधिकार रिट के विकास को उत्तर-औपनिवेशिक युग (पोस्ट कॉलोनियल एरा) में भारतीय संविधान में समाहित कर लिया गया, जहां इसके समावेशन के लिए प्रयास किए गए तथा न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन किया गया था।
रिट के प्रकार क्या हैं?
आइये अब हम बहुत महत्वपूर्ण उपकरण यानि रिट के वर्गीकरण पर चर्चा करें। नीचे पांच प्रकार के रिट, उनके अंतर्गत प्रचलित मामले और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट
‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ का शाब्दिक अर्थ है “आपको शरीर प्राप्त होगा”, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। रिट का यह वर्गीकरण उन परिस्थितियों में कानूनी उपाय प्रदान करता है जहां किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया जाता है, या किसी औपचारिक कानूनी या उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में रखा जाता है। यह रिट किसी व्यक्ति को ऐसी अवैध हिरासत से मुक्त होने तथा एक व्यक्ति के रूप में सम्मान के साथ जीने के अधिकार का आनंद लेने की अनुमति देती है।
न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे हिरासत पर कार्रवाई करने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त उचित साक्ष्य के आधार पर हिरासत की वैधता की जांच करेगा। केवल इसी आधार पर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करेगा तथा निर्णय करेगा कि क्या ऐसी हिरासत अवैध है या नहीं, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना गैरकानूनी था तथा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो न्यायालय को तत्काल जमानत पर रिहा करने का अधिकार है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और आपराधिक प्रक्रिया कानून की भ्रांतियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करके उसे प्राधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से शक्ति का दुरुपयोग करने से बचाता है। इसलिए, इसे राज्य प्राधिकारियों और व्यक्ति के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा का मौलिक अधिकार स्थापित करता है। यह अनुच्छेद किसी भी आधार या उचित स्पष्टीकरण के अभाव में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने से प्राधिकारियों को रोकता है। अनुच्छेद में आगे यह भी प्रावधान है कि वैध हिरासत के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट लागू होती है, जो प्रवर्तन तंत्र के मुख्य अंगों में से एक है, अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32।
प्रयोज्यता
बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिट याचिका उस व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो, या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हो। वे कोई रिश्तेदार या करीबी परिचित हो सकते हैं। हालाँकि, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से पक्ष बनने वाला व्यक्ति प्रासंगिक होना चाहिए तथा घटना से असंबंधित तीसरा पक्ष नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल वास्तविक हिरासत के आधार पर ही दायर की जा सकती है, न कि केवल हिरासत की आशंका के आधार पर दायर की जा सकती है।
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 97, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 100 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान प्रावधान निर्धारित करती है। इस प्रावधान में कहा गया है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने की आशंका हो, तो उन्हें अपने अधिकृत अधिकार क्षेत्र में तलाशी वारंट जारी करने का अधिकार है। इस प्रावधान के तहत जारी वारंट के माध्यम से पुलिस को सशक्त किया जाता है, जो उन्हें कथित गैरकानूनी हिरासत के संबंध में पूछताछ करने और उन्हें अदालत के समक्ष उपस्थित कराने का अधिकार देता है। यह कानून व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण और प्राधिकारियों की मनमानी से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रासंगिक मामले
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला आदि आदि (1976)
तथ्य
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला आदि आदि (1976) का मामला विवादास्पद आपातकाल के कारण उभरा, जिसे वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित किया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव की निष्पक्षता और अखंडता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने चुनाव को चुनावी कदाचार पर आधारित बताते हुए रद्द कर दिया। इस चुनाव के रद्द होने से प्रधानमंत्री की शक्तिशाली स्थिति खतरे में पड़ गई और उनकी सीट और उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया, इसलिए छह साल के लिए पद से अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा पैदा हो गया।
प्रधानमंत्री ने अपनी स्थिति के सभी संभावित खतरों और अस्थिरता पर विचार करते हुए 26 जून 1975 को राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी। इस आपातकाल के कारण अनुच्छेद 14, 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त उनके प्रवर्तन तंत्र को निलंबित कर दिया गया।
मौलिक अधिकारों के निलंबन के कारण विपक्ष के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (मीसा) के तहत हिरासत में लिया गया। इस तरह की कथित अवैध हिरासत में एबी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई जैसे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता शामिल थे। अनुच्छेद 32 के निलंबन से उन्हें उनके मूल व्यक्तिगत अधिकार से वंचित कर दिया गया, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों ने हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के पक्ष में आदेश दिया।
मुद्दा
दो मुख्य मुद्दे उठाए गए, जो निम्नलिखित थे:
- क्या अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका इस मामले के तहत स्वीकार्य थी। यह मुद्दा अनुच्छेद 359(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के संबंध में उठाया गया है, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि क्या आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका वैध होगी या नहीं।
- इस मामले में मुख्य मुद्दों में से एक इस मामले के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा का दायरा था। यह मुद्दा न्यायिक समीक्षा की प्रयोज्यता के संबंध में उठाया गया था, यदि अनुच्छेद 226 के तहत रिट स्वीकार्य हो जाए।

निर्णय
इस मामले में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 359(1) के तहत, जब राज्य में आपातकाल लागू हो, तो व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य रिट के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का हकदार नहीं है। इसने आगे तर्क दिया कि मीसा की धारा 16A(9) की वैधता को बरकरार रखते हुए न्यायपालिका के पास मीसा के तहत हिरासत को वैध बनाने की न्यायिक समीक्षा या जांच का अधिकार नहीं है। न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 359 की आगे व्याख्या की गई तथा यह पाया गया कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करता है तथा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित किसी भी कार्यवाही को निलंबित करने की अनुमति देता है।
सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)
तथ्य
सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) मामले में, याचिकाकर्ता, जेल कैदी सुनील बत्रा ने कैदियों की कठोर जीवन स्थितियों और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में एक पत्र के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को धमकाया था। याचिकाकर्ता ने यह भी शिकायत की कि उसके एक कैदी को मुख्य वार्डन द्वारा प्रताड़ित किया गया तथा उसके रिश्तेदारों को पैसे ऐंठने के लिए वार्डन द्वारा धमकाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पत्र पर विचार करते हुए इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट और जनहित याचिका के रूप में माना था।
याचिकाकर्ता के मित्र को गुदा में गंभीर चोटें आईं और कथित तौर पर उसके गुदा में धातु की छड़ डालकर उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई। यह भी कहा गया कि उसे वार्डन की यौन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया तथा उसका यौन उत्पीड़न किया गया। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि बाकी जेल अधिकारियों ने पैसे के बदले में वार्डन के खिलाफ आरोपों से इनकार कर दिया और चोटों को उचित ठहराते हुए दावा किया कि ये चोटें उन्होंने स्वयं लगाई थीं।
मुद्दा
उठाए गए मुद्दे निम्नलिखित थे:
- क्या जेल के कैदियों को अन्य व्यक्तियों के समान स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हैं? इस मुद्दे को जेलों के भीतर अमानवीय स्थितियों से निपटने के लिए आगे रखा गया।
- दूसरा मुद्दा यह था कि क्या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर मौलिक अधिकार लागू थे।
- जेल अधिनियम 1894 की धारा 30 के बारे में भी मुद्दे उठाए गए, जिसमें मृत्युदंड की सजा मिलने पर कैदी की संपत्ति जब्त करने और उसे एकांत कारावास में रखने का प्रावधान है। इसमें अधिनियम की धारा 56 पर भी चर्चा की गई है, जिसमें जेलकर्मियों के लिए दंड का प्रावधान है। इन प्रावधानों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ उनके संरेखण के आधार पर सवाल उठाया गया था।
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उसके पास हस्तक्षेप करने और कैदियों के मौलिक अधिकारों को सुदृढ़ करने का अधिकार है। अदालत ने आगे कहा कि अधिकारियों को किसी भी तरह से कैदियों को प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं है, केवल इस आधार पर कि वे व्यक्तिगत रूप से बंदी हैं। अदालत ने कहा कि वे भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के समान हकदार हैं।
न्यायालय ने पुलिस विभाग को जेलों में मानवीय स्थिति बनाये रखने का भी निर्देश दिया। जेल अधिनियम, 1894 की धारा 30(2) के संबंध में उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि एकांत कारावास जेल अधिकारियों को अनावश्यक दंड और यातना देने की अनुमति नहीं देता है। न्यायालय ने जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए कहा कि जेल अधिनियम, 1894 की धारा 30(2) अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है।
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)
तथ्य
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) के मामले में, याचिकाकर्ता ए.के. गोपालन एक साम्यवादी (कम्युनिस्ट) नेता थे, जिन्हें सार्वजनिक भाषण देने के कारण हिरासत में लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने लोक व्यवस्था अधिनियम, 1949 के तहत उनके खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया। मद्रास उच्च न्यायालय ने भी हिरासत को अवैध घोषित किया था। याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसे भी इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जमानत नहीं मिली। इसके अलावा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक और रिट याचिका दायर की गई, जिसके विरुद्ध एक नया हिरासत आदेश पारित किया गया।
याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32(1) के तहत रिट याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उन्होंने हिरासत को चुनौती देते हुए दावा किया कि यह गैरकानूनी और मनमानी है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या निवारक निरोध अधिनियम, 1950, अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 सहित संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है।
- क्या निवारक निरोध अधिनियम की धारा 3(1) के तहत जारी आदेश से अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
- क्या निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के प्रावधान अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुरूप हैं।
- क्या भारतीय संविधान की अभिव्यक्ति ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ अमेरिकी संविधान में प्रदत्त ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ के अर्थ से संबद्ध है।
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निवारक निरोध अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रतिकूल नहीं है। यह देखा गया कि अनुच्छेद 19(1) उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जिनकी स्वतंत्रता कानूनी रूप से प्रतिबंधित है और इसलिए, यह लागू करने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप, निवारक निरोध अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है।
हालाँकि, पीठ का बहुमत कनिया सी.जे., न्यायाधीश मुखर्जी, न्यायाधीश दास और पतंजलि शास्त्री जे.जे. द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्होंने कहा कि निवारक निरोध अधिनियम की धारा 14 असंवैधानिक है, यह तर्क देते हुए कि यह अनुच्छेद 22 (5) और 19 (5) का उल्लंघन करती है। यद्यपि सम्पूर्ण अधिनियम को शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु उल्लंघन करने वाले प्रावधान को सम्पूर्ण अधिनियम से अलग किया जा सकता है। अदालत ने अधिनियम की धारा 3, 7 और 11 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो सरकार को व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देती है।
इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 एक मूलभूत अधिकार है और अनुच्छेद 19 के दृष्टिकोण से ‘व्यक्तिगत स्वतंत्रता’ की व्याख्या भारतीय क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता के रूप में की तथा माना कि इस मामले में ऐसा अधिकार अन्य स्वतंत्रताओं तक विस्तारित नहीं होता है। इसने आगे दोहराया कि इस अनुच्छेद में भौतिक रूप में स्वतंत्रता शामिल है तथा इसका दायरा सीमित है। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अनुच्छेद 22(7)(b) के तहत हिरासत की न्यूनतम अवधि निर्धारित करने के लिए संसद द्वारा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है।
श्रीमती नीलाबती बेहरा उर्फ ललित बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1993)
तथ्य
श्रीमती नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य एवं अन्य (1993) मामले में याचिकाकर्ता नीलाबती बेहरा ने सर्वोच्च न्यायालय को एक पत्र लिखा, जब उसने अपने अभियुक्त बेटे सुमन बेहरा को रेलवे पटरियों पर मृत पाया था। याचिकाकर्ता के बेटे को पुलिस ने एक दिन पहले चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र में दावा किया कि उसके बाईस वर्षीय बेटे की पुलिस द्वारा दी गई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे लिखे गए पत्र की व्याख्या अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के रूप में की और मामले को आगे बढ़ाया था।

मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या याचिकाकर्ता का हिरासत में हिंसा और मौत का दावा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वैध और स्वीकार्य है।
- क्या राज्य क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी था, और यदि हाँ, तो किन कानूनी सिद्धांतों के तहत उत्तरदायी था। इस मुद्दे को आगे उठाया गया, तथा सार्वजनिक दायित्व और अपकृत्य (टॉर्ट) कार्रवाई के तहत निजी कानून द्वारा लगाए गए दायित्व के बीच अंतर को रेखांकित किया गया।
- संप्रभु प्रतिरक्षा के सिद्धांत के अस्तित्व के कारण, क्या संवैधानिक न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए आर्थिक मुआवजा देने का अधिकार है?
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के बेटे की मौत पुलिस हिरासत में रहने के दौरान हुई थी और पुलिस हिरासत में हुई उसके बेटे की मौत के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजा देने की अनुमति दी। इस मामले में प्रतिवादी उड़ीसा राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया तथा उसे याचिकाकर्ता नीलाबती मेहरा को 1,50,000 रुपये की धनराशि अदा करने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 32 के आधार पर अदालत द्वारा दिया गया मुआवजा, या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा, सार्वजनिक कानून उपचार की एक शाखा है, जो पूरी तरह से सख्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। इस मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। इस मामले में अदालत ने निजी और सार्वजनिक कानून के तहत दोनों प्रकार के उपचारों के बीच अंतर पर भी प्रकाश डाला।
रुदुल साह बनाम बिहार राज्य और अन्य (1983)
तथ्य
रुदुल साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1983) के मामले में याचिकाकर्ता रुदुल साह ने सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने झूठे कारावास के आधार पर अपनी रिहाई की प्रार्थना की थी। उन्होंने दावा किया कि चौदह वर्ष की कैद उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता पर वर्ष 1953 में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था और बाद में उसे दोषी ठहराया गया था। हालाँकि, 1968 में मुजफ्फरपुर सत्र न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के बाद भी उन्हें वर्ष 1982 तक जेल में ही रहना पड़ा था।
याचिकाकर्ता ने अपनी रिहाई की प्रार्थना करते हुए तर्क दिया कि उसे चौदह वर्षों तक गलत कारावास का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अदालत से अन्य सहायक राहतें भी प्रदान करने की अपील की, जैसे कि उनके पुनर्वास और स्वास्थ्य लाभ के लिए मौद्रिक प्रतिपूर्ति, चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिपूर्ति, तथा पूरी अवधि के दौरान उनकी अवैध हिरासत के लिए आर्थिक मुआवजा।
अदालत ने याचिकाकर्ता की सहायक राहतों के संबंध में मांगों पर विचार किया और राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जो इन दावों पर केंद्रित था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मुजफ्फरपुर केंद्रीय जेल के जेलर ने याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने के दो कारण बताए, जो थे;
- सबसे पहले, यह निर्णय लिया गया कि बरी करने के आदेश के बावजूद, मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा याचिकाकर्ता को राज्य सरकार और बिहार के जेल महानिरीक्षक के अगले निर्देश तक हिरासत में रखने का आदेश पारित किया गया था।
- दूसरे, जेलर ने दावा किया कि याचिकाकर्ता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और आगे कोई भी आदेश दिए जाने से पहले उसे हिरासत से रिहा नहीं किया जा सकता।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजा देने का अधिकार है।
- क्या अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजे का अधिकार शामिल है।
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की चौदह वर्ष की हिरासत को अवैध और अनुचित माना तथा उसका दावा सही था। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जीने की स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, और याचिकाकर्ता की रिट को अस्वीकार करने से उसे पहले से अधिक आघात पहुंचेगा, और उसने अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने अनुच्छेद 32 में निहित विवेकाधीन शक्ति और प्राधिकार के महत्व पर भी जोर दिया था।
न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि उल्लंघन किए गए अधिकारों और उल्लंघन करने वाले द्वारा अनिवार्य मुआवजा दिया जाना चाहिए, भले ही वह इकाई राज्य ही क्यों न हो। इसमें यह भी कहा गया कि ऐसे अधिकार से इनकार करना सार्वजनिक हित तथा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण के विपरीत होगा।
अदालत का यह भी मानना था कि याचिकाकर्ता को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और राज्य की कार्रवाई में याचिकाकर्ता की अवैध हिरासत के संबंध में कोई आधार और उचित तर्क का अभाव था। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए सहायक अधिकारों को भी वैध माना तथा उन्हें प्रदान कर दिया था।
कस्तूरीलाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1964)
तथ्य
कस्तूरीलाल रलिया राम जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1964) के मामले में, जो एक व्यापारी था, उसे पुलिस ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने कुछ मूल्यवान सामानों के साथ यात्रा कर रहा था, जिसमें काफी मात्रा में सोना भी शामिल था। पुलिसकर्मियों ने उनका रास्ता रोककर उन वस्तुओं को जब्त कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। याचिकाकर्ता ने अपना बचाव करते हुए कहा कि ये मूल्यवान वस्तुएं उसकी कंपनी की संपत्ति हैं, तथा इसके बावजूद उसे हिरासत में रखा गया है। अगले दिन कस्तूरी लाल को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके सभी कीमती सामानों में से केवल चांदी के सामान ही उन्हें लौटाए गए, जबकि सोना मांगने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया।
इसके बाद, कस्तूरी लाल ने मुकदमा दायर कर सोना वापस दिलाने या उसके मूल्य के बराबर मुआवजे की मांग की। अपना बचाव प्रस्तुत करने पर राज्य ने सभी आरोपों से इनकार किया तथा कीमती सोना दिखाने या याचिकाकर्ता को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आगे तर्क देते हुए कहा कि सोना तत्कालीन हेड कांस्टेबल श्री आमिर के पास रखा गया था, जिन्होंने सभी कीमती सामान ‘पुलिस मालखाना’ में जमा कर दिया था, जो बाद में फरार हो गया और पाकिस्तान भाग गया। राज्य ने यह भी कहा कि हेड कांस्टेबल श्री आमिर के खिलाफ कई कार्रवाई करने के बावजूद उनका पता नहीं लगाया जा सका और उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सका।
उत्तर प्रदेश की विचारण न्यायालय ने राज्य को उत्तरदायी माना और कस्तूरी लाल को 11,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। राज्य विचारण न्यायालय के फैसले से व्यथित था और उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने विचारण न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया और प्रतिवादी के तर्कों का समर्थन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस की कथित लापरवाही के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इसने आगे कहा कि लापरवाही की धारणा के आधार पर भी, याचिकाकर्ता की ओर से राज्य से आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग करना अनुचित था। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया, जहां याचिकाकर्ता ने अपील की थी।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या पुलिसकर्मी वास्तव में कस्तूरी लाल की संपत्ति, विशेषकर सोने के प्रति अपने कार्यों और जिम्मेदारियों में लापरवाह थे।
- क्या राज्य याचिकाकर्ता के सोने के सामान के संबंध में हेड कांस्टेबल श्री आमिर की लापरवाही के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
निर्णय
अपना फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया (1861) 5 बॉम एच.सी.आर. ऐप. I, पृ.1 नामक मामले का हवाला दिया। यह मामला लोक सेवकों के प्रतिस्थानिक (वायकेरियस) दायित्व (एक दायित्व जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है) से संबंधित है। उस मामले में, राज्य को संप्रभु प्रतिरक्षा प्रदान की गई थी, तथा याचिका को खारिज करते हुए राज्य के विरुद्ध प्रतिस्थानिक रूप से उत्तरदायी होने के दावे को अस्वीकार कर दिया गया था। वर्तमान मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले के रेशियो डिसिडेंडी का संदर्भ दिया, तथा माना कि राज्य हेड कांस्टेबल, श्री आमिर के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है।
हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस अधिकारियों ने कस्तूरी लाल के सामान को अपने संरक्षण में रखने में वास्तव में लापरवाही बरती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि संपत्ति को लापरवाही से पुलिस हिरासत में रखा गया था और इस मुद्दे को अपीलकर्ता के पक्ष में संबोधित किया था।
अगले मुद्दे पर विचार करते हुए, जो राज्य की संप्रभु प्रतिरक्षा से संबंधित था, न्यायालय ने ऊपर वर्णित उसी मामले का संदर्भ दिया तथा अपने निर्णय के पीछे के तर्क का अनुसरण किया। इसने माना कि राज्य को अपनी संप्रभु शक्तियों के कारण छूट प्राप्त है, और इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध दावे को अस्वीकार कर दिया गया।
इस मामले में न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी की गई, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों में से एक साबित हुई। कस्तूरीलाल रलिया राम जैन के अधिकारों के उल्लंघन को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से संबोधित किया गया था, जहां यह दावा किया गया था कि वैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया गया था क्योंकि उन्हें और उनके मूल्यवान सामानों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।
परमादेश रिट
‘परमादेश’ का शाब्दिक अर्थ है ‘आदेश देना’। रिट के इस विविधीकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति, निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकारी या सरकार को उनके संबंधित सार्वजनिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों जिन्हें पूरा करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हैं को पूरा करने के लिए बाध्य करने के लिए आदेश या निर्देश जारी करना है। जो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित होते हैं, उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में परमादेश रिट जारी करने के लिए अपील करने का अधिकार है।
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए तथा किसी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण को ऐसी कार्रवाई करने से रोकने के लिए परमादेश रिट जारी कर सकता है, जो किसी व्यक्ति और उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।
इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय को कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए परमादेश रिट जारी करने का अधिकार है, और ये उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसमे शामिल है:
- किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य मुद्दों पर ध्यान देने वाले निर्देश।
- उच्च न्यायालय को परमादेश रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, जो किसी पद पर आसीन व्यक्ति के लिए असंवैधानिक तथा बाध्यकारी कार्यों से संबंधित है।
- उच्च न्यायालय किसी न्यायाधिकरण की निचली अदालत को अपने इनकार के संबंध में अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दे सकता है, तथा उन मामलों पर विचार कर सकता है जहां कोई सार्वजनिक अधिकारी दुर्भावनापूर्ण, गैरकानूनी तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है तथा अपने विवेकाधीन अधिकार का दुरुपयोग करता है।
परमादेश रिट जारी करने से पहले कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
- सबसे पहले, जिस व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ रिट जारी की जाती है, उसके पास कोई सार्वजनिक कर्तव्य होना चाहिए, जिसे पूरा करने में वे विफल रहे हों। ऐसा कर्तव्य विवेकाधीन न होकर अनिवार्य प्रकृति का होना चाहिए।
- दूसरा जो व्यक्ति परमादेश रिट की मांग कर रहा है, उसके पास सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने का अधिकार होना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को न्यायालय से अधिकारी के विरुद्ध परमादेश रिट मांगने से पहले ही सार्वजनिक अधिकारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अनुरोध करना चाहिए था।
परमादेश के प्रकार
परमादेश रिट को जारी करने और निष्पादन की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
प्रमाणित परमादेश
इस प्रकार की रिट, परमादेश रिट और उत्प्रेषण रिट का मिश्रण है। इस प्रकार के रिट में, किसी निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जाती है, जहां ऐसा निर्णय पहले ही किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका हो। उत्प्रेषण रिट, किसी निश्चित कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अत्यधिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों में पारित की जाती है। कुछ परिस्थितियों में, परमादेश और उत्प्रेषण रिट में टकराव हो सकता है, जहां परमादेश रिट को उस मामले को पुनः सुनने का अधिकार होगा, जिसे पहले उत्प्रेषण रिट द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

अनुमेय परमादेश
अनुमेय का अर्थ है, कुछ ऐसा जो निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) हो, दृढ़ हो और जिस पर बहस न हो सके, तथा जो कहा जा सके वह उसके अंतिम निर्णय में निहित हो। इसी प्रकार, एक अनिवार्य आदेश की प्रकृति का रिट न्यायालय द्वारा सरकारी एजेंसियों या किसी सार्वजनिक अधिकारी को बिना किसी चूक के अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश होता है।
इस प्रकार का रिट वैकल्पिक परमादेश से भिन्न होता है। ऐसे मामलों में जहां अधिकारी न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तथा न्यायालय को इस बात से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं कि रिट को अस्वीकार क्यों किया जाना चाहिए, तो न्यायालय द्वारा परमादेश रिट जारी की जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, जहां आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा हो सकता है कि वैकल्पिक रिट जारी किए बिना ही सरकारी अधिकारियों को इसका अनुपालन करने का निर्देश देते हुए एक अनिवार्य रिट जारी की जा सकती है।
जारी परमादेश
कुछ परिस्थितियों में, परमादेश जारी करने के बाद अनिवार्य अनुवर्ती (फॉलो-अप) कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया की प्रकृति की होती है। ऐसा उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, न्यायालय उस प्राधिकारी से समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट की मांग कर सकता है, जिसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी की गई है। इस तरह की रिट यह सुनिश्चित करती है कि अदालत के आदेश न केवल जारी किए जाएं बल्कि उनका परिश्रमपूर्वक और सक्रिय रूप से पालन भी किया जाए।
परमादेश रिट पर प्रासंगिक मामले
एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1982)
तथ्य
वर्ष 1981 में भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में वकीलों और विधि विशेषज्ञों द्वारा कई याचिकाएं दायर की गईं। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1982) मामले में याचिकाकर्ताओं ने दो न्यायाधीशों की नियुक्ति न किये जाने तथा उनके हस्तांतरण के संबंध में याचिकाएं दायर की थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में तर्क दिया गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया असंवैधानिक है।
यह मुद्दा मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की अल्प-नियुक्ति के कारण उठाया गया था, जिसके बारे में दावा किया गया था कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत न्यायोचित नहीं है। इन याचिकाकर्ताओं में एस.पी. गुप्ता भी एक थे, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील थे। उन्होंने तीन न्यायाधीशों, अर्थात् न्यायमूर्ति मुरलीधर, न्यायमूर्ति ए.एन. वर्मा और न्यायमूर्ति एन.एन. मित्तल की नियुक्ति के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिकाओं में किए गए दावों और तर्कों का बचाव प्रतिवादी ने यह तर्क देकर किया कि सरकार का आदेश और न्यायाधीशों की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है और इससे किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण न करने का केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेश संवैधानिक रूप से वैध था।
- इनमें से एक मुद्दा विधि मंत्री, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बीच संवाद से संबंधित था।
- क्या याचिकाकर्ता इस मामले को अदालत में लाने के लिए हकदार और अधिकृत थे।
- इनमें से एक मुद्दे में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उच्च मंचों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया।
निर्णय
इस निर्णय में न्यायमूर्ति भगवती द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों के लिए राष्ट्रपति को उम्मीदवारों की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक कॉलेजियम के गठन की सिफारिश की गई थी। ‘परामर्श’ के अर्थ की व्याख्या करते हुए, न्यायाधीशों ने व्याख्या की कि इसका तात्पर्य सार्थक आदान-प्रदान से है, और सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति वेंकटरामैया ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 217 में भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। हालाँकि, यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को कुछ प्राधिकारियों से परामर्श अवश्य करना होगा, लेकिन वह उनके सुझावों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
न्यायालय ने कहा कि यदि कार्यपालिका को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया तो न्यायपालिका अपना महत्व खो देगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित रखा जा सकेगा।
सुगनमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (1965)
तथ्य
सुगनमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (1965) के मामले में, अपीलकर्ता इंदौर में भंडारी आयरन एंड स्टील कंपनी का प्रबंध मालिक था और उसने इंदौर औद्योगिक कर अधिनियम, 1927 के तहत प्रावधानित (प्रोविजनड) औद्योगिक कर का भुगतान किया था। कपास मिलिंग के व्यवसाय में शामिल न होने के बावजूद भी कंपनी को कर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, कंपनी ने दो अग्रिम भुगतान किए, जिनका भुगतान करने के लिए वे उत्तरदायी नहीं थे, और उन्होंने न्यायालय में अपील की, जबकि अंतिम कर निर्धारण वर्ष 1951-1952 में गणना की गई थी। अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और यह माना कि कंपनी औद्योगिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए कर भुगतान वापस करने से इनकार कर दिया गया। अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार से धन वापसी का अनुरोध किया और बदले में उसे आंशिक भुगतान किया गया।
अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट दायर कर राज्य सरकार को कंपनी को शेष धनराशि वापस करने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य कंपनी को कर राशि वापस करने के लिए बाध्य नहीं है और यह भी कहा कि इस तरह के निष्पादन का आदेश देना अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय था।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या इस मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर परमादेश रिट स्वीकार्य थी।
- क्या राज्य का कंपनी द्वारा आंशिक रूप से भुगतान की गई कर राशि को वापस करने का वैधानिक दायित्व था।
- क्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का कंपनी की अपील को खारिज करने तथा कर राशि की वापसी भुगतान की दलीलों को अस्वीकार करने का निर्णय विधिक और तथ्यात्मक रूप से सही था।
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे में रिट जारी करने की शक्ति है। हालाँकि, वह याचिका जो केवल राज्य को धन वापस करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश रिट की मांग करती है, स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता इस बात की जांच के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि क्या कर निर्धारण संविधान का उल्लंघन है। इस उदाहरण का समर्थन न्यायालय ने यह कहते हुए किया कि कर वापसी का दावा केवल सिविल मुकदमे के माध्यम से ही स्वीकार्य है तथा परमादेश रिट राज्य को कर राशि वापस करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।
संगीता विलास इंगले बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2017)
तथ्य
संगीता विलास इंगले बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2017) के मामले में, अपीलकर्ता को पहले तो पुलिसकर्मियों और अन्य प्राधिकारियों से यातना और गैरकानूनी कार्यों का सामना करना पड़ा, जिसके खिलाफ उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास अन्य उपाय भी हैं, तथा कथित शिकायतें इतनी व्यवहार्य हैं कि उन्हें रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के बजाय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जा सकता है। बाद में इस मामले को आगे की अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया गया था।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा केवल तथ्यों के विवादित प्रश्न के आधार पर रिट याचिका को खारिज करना न्यायोचित था।
- क्या बॉम्बे उच्च न्यायालय को याचिका खारिज करने से पहले उसके सभी अंतर्निहित गुणों की जांच करनी चाहिए थी।
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई, जिसमें पाया गया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने केवल विवादित तथ्यों के आधार पर अपील को खारिज करके कानून के साथ अन्याय किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति के संबंध में मामले के सभी गुण-दोषों का विश्लेषण करना चाहिए था। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने शीघ्र सुनवाई का निर्देश भी जारी किया तथा मामले के गुण-दोष की जांच की तथा सुझाव दिया कि इसका निपटारा एक वर्ष के भीतर किया जाए।

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम नूरुद्दीन मलिक और अन्य (1998)
तथ्य
पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम नूरुद्दीन मलिक और अन्य (1998) के मामले में, पश्चिम बंगाल में बिशालक्ष्मीपुर पुणे शाह मस्तानिया जूनियर हाई मदरसा नामक एक मदरसा छात्रों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता था, विशेष रूप से कक्षा V से VII तक। बाद में, इस शैक्षणिक संस्थान ने अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार और उन्नयन करने का इरादा किया, जिसमें उच्च शिक्षा (एक उच्च मदरसा) शामिल थी, जिसमें कक्षा V से X तक और कक्षा IX-X शामिल थे। यह विस्तार सक्षम अधिकारियों से किसी पूर्व अनुमोदन या मंजूरी के बिना किया गया था। समय के साथ, मदरसा ने अपने प्रशासन का विस्तार किया, और कक्षा IX-X के लिए छात्रों के नामांकन के साथ-साथ उनके कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी। विस्तार के संबंध में कोई पूर्व अनुमोदन न होने के बावजूद, बोर्ड ने छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी।
बाद में, कलकत्ता उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें मदरसा प्राधिकारियों को मदरसा को उच्च मदरसा के रूप में मान्यता देने का आदेश देने की प्रार्थना की गई। बाद में यह मामला निर्णय हेतु सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भेज दिया गया था।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या प्राधिकारियों के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जिनमें प्रधानाध्यापक भी शामिल हैं, को उनके संबंधित पदों पर विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करना अनिवार्य था।
- क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड को सभी कर्मचारियों की सेवाओं को अनुमोदित करने तथा निर्धारित अवधि के भीतर उनका वेतन जारी करने का आदेश देना सही था?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया तथा कहा कि कर्मचारी सदस्यों तथा अन्य प्रशासनिक नौकरियों की भर्ती के दौरान प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का उचित पालन होना चाहिए। इसने आगे पाया कि मदरसे द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी सदस्यों के लिए मांगी गई स्वीकृति, स्वीकृत कर्मचारी स्वरूप से अधिक थी। अदालत ने आगे कहा कि कई प्रस्तावित कर्मचारी अपेक्षित योग्यताएं पूरी नहीं करते है।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अपने फैसले में प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की योग्यता की जांच करके तथा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन करके उनका अनुमोदन करें। अदालत ने अपने फैसले में प्राधिकारियों को चार महीने के भीतर निर्णय लेने तथा अनावश्यक देरी से बचने का आदेश दिया, जिससे संस्था के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
प्रतिषेध रिट
‘प्रतिषेध’ का शाब्दिक अर्थ रोकना’ या ‘निषेध करना’ या ‘नियंत्रित करना’ हो सकता है। कानूनी भाषा में, प्रतिषेध को ‘स्थगन आदेश’ कहा जा सकता है। ‘प्रतिषेध’ को एक कानूनी उपाय माना जाता है, जिसके तहत किसी निचली अदालत, प्रशासनिक निकाय या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय में अपील की जाती है।
मेरियम-वेबस्टर शब्दकोष में दी गई परिभाषा के अनुसार, प्रतिषेध रिट “एक उच्च न्यायालय द्वारा किसी निम्न न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया गया रिट है।” दूसरे शब्दों में, प्रतिषेध रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश या निर्देश है, जिसमें निचली अदालत को ऐसी कार्यवाही बंद करने का निर्देश दिया जाता है, जो उसके कानूनी अधिकार से परे हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हो। प्रतिषेध रिट का उद्देश्य त्रुटियों से सुरक्षा प्रदान करना तथा मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से होने वाले संभावित नुकसान को रोकना है।
प्रतिषेध रिट जारी करने के आधार
प्रतिषेध जारी करने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो इस प्रकार विस्तृत हैं:
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
यदि किसी व्यक्ति को दिए गए किसी अधिकार का उल्लंघन निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट (प्रोहिबिशन) जारी की जा सकती है। यद्यपि इसका उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि क्या किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार आदि।
असंवैधानिक या अधिकारातीत (अल्ट्रा वाइरस) कार्य
उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट उस स्थिति में जारी की जा सकती है जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण असंवैधानिक तरीके से काम करता है या अन्यथा उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है। इस प्रकार की रिट निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा किसी भी गैरकानूनी या संवैधानिक कार्य को रोकने के लिए मांगी जा सकती है।
साक्ष्य ठीक से प्राप्त नहीं किया गया
किसी न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट उन मामलों में जारी की जा सकती है, जहां निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय समुचित साक्ष्य के बिना या सत्य की उपेक्षा करके दिया गया हो। इस आधार में यह साबित करना शामिल है कि निचली अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण तथ्यात्मक त्रुटि पर आधारित है या साक्ष्य के गलत प्रस्तुतीकरण से निकला है।
प्रतिषेध रिट पर प्रासंगिक मामले
शेषांक सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1996)
तथ्य
शेषांक सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1996) के मामले में मेसर्स कामथ पैकेजिंग लिमिटेड ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रतिषेध रिट याचिका दायर की, जिसमें उनके गोदाम में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाने वाली तलाशी और जब्ती पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिकारियों को कच्चे माल के संबंध में जांच करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, जिन्हें शुल्क छूट योजना के तहत दिए गए अग्रिम अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के तहत आयात किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, प्राधिकारियों को इन मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं देता है।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या सीमा शुल्क अधिकारियों को कच्चे माल के उपयोग के संबंध में जांच करने तथा जब्ती एवं तलाशी अभियान चलाने के लिए अधिकृत किया गया था।
- क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ने सीमा शुल्क अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25(1) के तहत जारी अधिसूचित नियमों और शर्तों के अनुपालन को लागू करने का अधिकार दिया है।
- क्या सीमा शुल्क प्राधिकारियों को निर्यात नीति, 1988-91 और प्रक्रिया पुस्तिका, जिसमें शुल्क छूट योजना निहित है, के अनुसार छूट प्राप्त सामग्रियों की बिक्री या दुरुपयोग से संबंधित मामलों के संबंध में जांच करने की अनुमति थी।
- क्या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111(o), जो कुछ शर्तों के अधीन शुल्क से छूट प्राप्त वस्तुओं को जब्त करने का प्रावधान करती है, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को छूट अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करती है।
निर्णय
इस मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल और खंडपीठ, दोनों ने अपने फैसले में सीमा शुल्क अधिकारियों के कानूनी अधिकार को बरकरार रखा, ताकि वे कच्चे माल के आयात के लिए छूट की शर्तों को लागू करते हुए जांच और अनुपालन सुनिश्चित कर सकें। अदालत ने आगे कहा कि छूट अधिसूचना की शर्तों सहित अग्रिम अनुज्ञप्ति के बावजूद, आयातित कच्चे माल के उपयोग की जांच करने का अधिकार सीमा शुल्क अधिकारियों को है।

अदालत ने आगे कहा कि आयात और निर्यात नीति तथा प्रक्रिया पुस्तिका, छूट शर्तों के कथित उल्लंघन की जांच करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के नियंत्रण को कम नहीं करती है।
अधिकार पृच्छा रिट
लैटिन वाक्यांश ‘अधिकार पृच्छा’ का शाब्दिक अर्थ है ‘किस अधिकार या पृच्छा द्वारा’। रिट का यह वर्गीकरण ऐसे निर्देश या आदेश से संबंधित है जो किसी व्यक्ति के प्राधिकार या सार्वजनिक पद, स्थिति या मताधिकार रखने के अधिकार पर प्रश्न उठाता है। अधिकार पृच्छा रिट का प्रयोग किसी व्यक्ति के अधिकार या प्राधिकार को चुनौती देने के लिए किया जाता है, जो शक्तियों और अधिकारों से संबंधित विशिष्ट (स्पेसिफिक) पद पर आसीन होने के लिए होता है।
प्राचीन काल में, क्राउन ने सार्वजनिक कार्यालयों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा अनधिकृत व्यक्तियों को उन कार्यालयों पर कब्जा करने से रोकने के लिए अधिकार पृच्छा रिट का उपयोग एक तंत्र के रूप में किया था। समय के साथ, अधिकार पृच्छा रिट विकसित हुई जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक कार्यालय सही ढंग से अधिकृत हों।
अधिकार पृच्छा रिट मांगने के आधार
अधिकार पृच्छा के तहत आदेश या निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:
शक्ति का दुरुपयोग
न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार पृच्छा रिट जारी कर सकता है जो अपने प्राधिकार का दुरुपयोग कर रहा हो। न्यायालय को उस मामले की परिस्थितियों और मामलों की जांच करने के बाद उनके पद धारण करने के अधिकार पर सवाल उठाने का अधिकार है।
किसी अधिकृत व्यक्ति की अयोग्यता
यदि यह पाया गया हो कि पदधारी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो अधिकार पृच्छा रिट प्राप्त की जा सकती है। न्यायालय किसी व्यक्ति के पद धारण करने की वैधता पर प्रश्न उठा सकता है।
कार्यालय की दोहरी क्षमता
अधिकार पृच्छा रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है जो एक पदधारी है तथा एक साथ एक से अधिक पदों पर कार्य कर रहा है। न्यायालय रिट जारी करने से पहले उचित जांच कर सकता है, साक्ष्यों की जांच कर सकता है और उचित प्रक्रिया का पालन कर सकता है।
अधिकार पृच्छा रिट पर प्रासंगिक मामले
मैसूर विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम सी. डी. गोविंदा राव एवं अन्य (1963)
तथ्य
मैसूर विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम सी. डी. गोविंदा राव एवं अन्य (1963) के मामले में, याचिकाकर्ता सी. डी. गोविंदा राव ने अनुच्छेद 226 के तहत मैसूर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें अधिकार पृच्छा रिट जारी करने की प्रार्थना की गई। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय महाविद्यालय, बेंगलुरू में अंग्रेजी के शोध पाठक (रिसर्च रीडर) के रूप में अन्नया गौड़ा की स्थिति पर सवाल उठाया था।
याचिकाकर्ता ने शोध पाठक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक कुछ शर्तों की सूची प्रदान की, जिसमें किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि, समकक्ष; डॉक्टरेट स्तर पर शोध की उपाधि; स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का दस वर्ष (न्यूनतम 5 वर्ष) का अनुभव; क्षेत्रीय भाषा, कन्नड़ का ज्ञान, को भी प्राथमिकता दी गई। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि मौजूदा शोध पाठक अन्नया गौड़ा के पास इनमें से अधिकांश योग्यताएं नहीं थीं, इसलिए उन्हें इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया था।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- शोध पाठक के पद पर अन्नया गौड़ा की नियुक्ति की वैधता।
- क्या याचिकाकर्ता के पास महाविद्यालय में अंग्रेजी के शोध पाठक के पद के लिए सभी योग्यताएं थीं।
- क्या अधिकार पृच्छा की रिट उस प्राधिकार को प्रदर्शित करने के लिए स्वीकार्य थी जिसके तहत अनुसंधान पाठक अपना पद धारण कर रहा था।
- मैसूर विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता को शोध पाठक के रूप में नियुक्त करने का निर्देश देने वाले परमादेश रिट की स्थिरता थी।
निर्णय
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय महाविद्यालय में अंग्रेजी में शोध पाठक के रूप में अन्नया गौड़ा की नियुक्ति सभी योग्यताओं और भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। अदालत ने महाविद्यालय के आचरण की आलोचना की, विशेष रूप से सेवा रिकॉर्डों में विसंगतियों और अशुद्धियों के संबंध में, तथा अन्नया गौड़ा की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया था।
इस मामले को पीड़ित पक्ष अर्थात् अन्नया गौड़ा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आगे अपील की गई, जहां न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को खारिज कर दिया तथा अन्नया गौड़ा की नियुक्ति को वैध तथा पूरी तरह कानून सम्मत माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यद्यपि प्रारंभिक हलफनामे के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणी कुछ विसंगतियों के कारण उचित थी, लेकिन यह अपीलकर्ता की नियुक्ति की वैधता पर बहुत कठोर थी। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय को प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना चाहिए था, जिसमें अपीलकर्ता का विस्तृत हलफनामा भी शामिल था, जिसमें आवश्यकताओं के अनुरूप उसकी सभी योग्यताएं सूचीबद्ध थीं।
उत्प्रेषण रिट
उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है ‘प्रमाणित होना’ या ‘सूचित होना’, जिसका अर्थ लैटिन शब्द से लिया गया है। यह रिट की एक श्रेणी है जो किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा निचली अदालत या अधीनस्थ अदालतों, न्यायाधिकरणों या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दिए गए पिछले निर्णय की अमान्यता को प्रमाणित करने के लिए जारी की जाती है।
उत्प्रेषण की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, “किसी अवर न्यायालय या अर्ध-न्यायिक क्षमता में कार्यरत निकाय के अभिलेखों को मंगाने के लिए उच्च न्यायालय की रिट।” इसके अलावा, यह वैधानिक निकायों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, चाहे वे अपनी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक क्षमता का प्रयोग कर रहे हों। इस रिट का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना है कि निचली अदालत या प्रशासनिक प्राधिकारियों ने कानून की व्याख्या करते समय उसे सही ढंग से लागू किया है या नहीं। उत्प्रेषण रिट की अवधारणा इंग्लैंड के सामान्य कानून से उभरी है, जबकि इसकी उत्पत्ति मेडिकल इंग्लैंड में मानी जाती है।
स्वतंत्रता से पहले, भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालयों को व्यापक शक्तियां प्रदान कीं, जिससे उन्हें किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए उत्प्रेषण रिट के माध्यम से निर्देश जारी करने का अधिकार मिला है।
उत्प्रेषण रिट मांगने के कारण
उत्प्रेषण रिट के तहत आदेश या निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:
अधिकार-क्षेत्र संबंधी त्रुटि
उत्प्रेषण रिट किसी न्यायालय द्वारा उस स्थिति में जारी की जा सकती है जब निचली अदालतें उसके प्राधिकार का अतिक्रमण करती हैं या ऐसे प्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहती हैं।
कानून की त्रुटि
यदि किसी मामले में किसी पक्ष को यह लगता है कि न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गई है, तो ऐसा पक्ष उच्चतर मंच से उत्प्रेषण रिट जारी करने की प्रार्थना कर सकता है। ऐसी त्रुटियों के कारण अन्यायपूर्ण या महत्वपूर्ण रूप से गलत निर्णय हो सकता है, जिससे समता, न्याय और उनके मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकते हैं, और इसलिए उत्प्रेषण रिट जारी करना एक रास्ता है।
कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न
किसी मामले को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उसमें विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए। कोई उच्च मंच या न्यायालय, किसी असाधारण मामले को छोड़कर, नये साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता तथा तथ्यों और परिस्थितियों की जांच नहीं कर सकता। किसी मामले के साक्ष्य का विश्लेषण करने के लिए न्यायालय को तभी प्राधिकृत किया जाता है, जब उससे कोई सारवान कानूनी प्रश्न जुड़ा हो। कानून के ऐसे सारवान प्रश्न में किसी वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान या किसी ऐसे महत्व की बात की व्याख्या शामिल होती है जो न्याय और समता के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो।
विवादित निर्णय
ऐसे मामलों में जहां उच्च न्यायालयों के निर्णयों में विरोधाभास हो, उच्च मंच द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकती है। उच्च मंच द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देश में मामले, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और दलीलों तथा न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का विश्लेषण करने की शक्ति होगी। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, कोई अदालत उच्च न्यायालयों के बीच विवादों को खारिज करते हुए अपना फैसला सुना सकती है।
प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन
प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के किसी मामले में, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बहाल करने के लिए परमादेश रिट जारी की जा सकती है। ये उल्लंघन जबरदस्ती, धोखाधड़ी या मिलीभगत जैसे कारकों के कारण हो सकते हैं।
न्यायिक समीक्षा
न्यायिक समीक्षा करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। रिट का यह वर्गीकरण भारतीय न्यायिक प्रणाली द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तारित करने की अनुमति देता है।
उत्प्रेषण रिट पर प्रासंगिक कानूनी मामले
के.वी.एस.राम बनाम बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (2015)
तथ्य
के.वी.एस. राम बनाम बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (2015) के मामले में, अपीलकर्ता पर धोखाधड़ीपूर्ण हस्तांतरण प्रमाणपत्र के माध्यम से अपना पद प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में चालक (ड्राइवर) के रूप में काम करता था। अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों के संबंध में जांच शुरू की गई थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अपीलकर्ता की नियुक्ति फर्जी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त की गई थी।
मुद्दा
इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:
- क्या अपीलकर्ता को बैंगलोर महानगर परिवहन निगम में चालक के पद से बर्खास्त करना उचित था। इस मुद्दे में इस बात की समीक्षा शामिल है कि क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया है तथा दंड लगाने में उचित प्रक्रिया का पालन किया है।
- क्या बर्खास्तगी की सजा अपीलकर्ता के कथित कदाचार के अनुरूप थी।
- क्या कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले, एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों द्वारा, न्यायोचित और कानूनी रूप से सत्य थे।
निर्णय
इस मामले को न्यायिक समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बर्खास्तगी की पुष्टि करने का उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय गलत था। इसने आगे कहा कि जांच में अत्यधिक देरी, अपीलकर्ता की आयु, तथा यह तथ्य कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को कम दंड दिया गया था, ये सभी बातें श्रम न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को कम दंड के साथ बहाल करने के निर्णय के अनुरूप थीं।
इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि श्रम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11A के तहत अपने विवेक का उचित प्रयोग किया था, जो श्रमिकों की बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के मामले में उचित राहत देने के लिए श्रम न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की शक्तियों का प्रावधान करता है। इसलिए, उसने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, श्रम न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया और अपीलकर्ता की बहाली का आदेश दिया था।

रिटों का अवलोकन
| रिट | विवरण | जारी करने का प्राधिकारी | यह किसके विरुद्ध जारी की जा सकती हैं ? | किसके विरुद्ध यह जारी नहीं की जा सकती हैं |
| बंदी प्रत्यक्षीकरण | बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है “आपको शरीर मिलेगा”। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त करने तथा उस व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी से पूछताछ करने के लिए जारी की जाती है। | सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय | कोई भी सार्वजनिक या निजी व्यक्ति या प्राधिकारी, जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले रहा हो। | निम्नलिखित मामले हैं जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी नहीं की जा सकती है:
|
| परमादेश | ‘परमादेश’ का शाब्दिक अर्थ है ‘आदेश देना’। यह रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय या किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु जारी की जाती है। | सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय | सार्वजनिक अधिकारी, अधीनस्थ एवं निचली अदालतें, सरकारी निकाय जो सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य हैं। | परमादेश रिट राज्य के प्रमुख, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती।
परमादेश रिट किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी नहीं की जा सकती। |
| प्रतिषेध | प्रतिषेध रिट न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। | सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय | निचली एवं अधीनस्थ अदालतों, न्यायाधिकरणों या अर्ध-न्यायिक निकायों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करना। | प्रतिषेध किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। |
| उत्प्रेषण | उत्प्रेषण का मूलतः अर्थ है “प्रमाणित होना”। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों के निर्णय की समीक्षा करने और उसे रद्द करने के लिए जारी की जाती है, यदि वह ऐसा करना उचित समझे। | सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय | निचली या अधीनस्थ अदालतें, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण। | उत्प्रेषण रिट विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी नहीं जा सकती है। |
| अधिकार-पृच्छा | “अधिकार-पृच्छा” का अर्थ है “किस अधिकारी द्वारा”। यह रिट न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति को बुलाने और उससे यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किस प्राधिकार के तहत ऐसा पद धारण कर रहा है। | सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय | कोई व्यक्ति जो कानूनी अधिकार के बिना सार्वजनिक पद पर आसीन है। | अधिकार-पृच्छा रिट किसी निजी कार्यालय और कानूनी रूप से सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। |
संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका
न्यायिक सक्रियता एक दर्शन है, जो मिसालों और मिसाली विश्लेषण से जुड़ा है। यह विभिन्न निर्णयों के माध्यम से मामलों और कानूनी मुद्दों को संबोधित करने की एक विधि है, जो सामान्य कानूनों और नियमों से परे हैं। न्यायिक सक्रियता का अस्तित्व राज्य की कार्रवाई की समीक्षा करने की अदालतों की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। न्यायालयों को ऐसी शक्तियां अनुच्छेद 13 से प्राप्त हुई हैं, जिसे अनुच्छेद 32 और 226 के साथ पढ़ा जाए, जहां भारतीय संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को हमारे ऊपर शासन करने वाले कानूनों की व्याख्या करने की अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उर्वरक (फर्टिलाइजर) निगम कामगार संघ (पंजीकृत), सिंदरी एवं अन्य बनाम भारत संघ (1981) के मामले में माना कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति भारतीय संविधान की मूल संरचनाओं में से एक है।
न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सुलभ होना चाहिए। न्याय तक उचित पहुंच के बिना शासन की स्थापना संभव नहीं है। न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं के संबंध में प्रगति करके खुद को पीछे छोड़ दिया है। जनहित याचिका के माध्यम से, भारतीय न्यायपालिका ने निर्धन लोगों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों, मानव तस्करी से पीड़ित लोगों, ट्रांसजेंडरों और कई अन्य लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
इसके अलावा, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के महत्व को बरकरार रखा और कहा कि यह पारंपरिक प्रतिकूल न्याय प्रणाली से खुद को अलग करता है। न्यायालय ने जनहित याचिका के लाभों पर विचार करते हुए कहा कि इसका आविष्कार समाज के मुद्दों को संबोधित करने में आगे बढ़ता है, जो एक तरह से संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और उसके उपचारों पर केंद्रित है।
जैसा कि हम देख सकते हैं कि जनहित याचिका एक व्यक्ति और पूरे समाज के संवैधानिक उपचारों का जवाब देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आइए इसके महत्व को समझने के लिए इस पर विस्तार से चर्चा करें।
जनहित याचिका क्या है?
जनहित याचिका (पीआईएल) को मोटे तौर पर ‘सार्वजनिक हित की रक्षा के उद्देश्य से दायर मुकदमे’ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य उन व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करना और कम करना है जिनके साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष न्यायिक कार्यवाही आवश्यक है। जनहित याचिका एक नया कानूनी ढांचा तैयार करती है, जो राज्य को संवैधानिक और कानूनी उल्लंघनों के लिए जवाबदेह बनाती है, जो समाज के सदस्यों, विशेषकर कमजोर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
1960 और 1970 के दशक तक भारत में मुकदमेबाजी अभी भी अपने शुरुआती चरण में थी, जिसे मुख्य रूप से व्यक्तियों द्वारा अपने निजी हितों को आगे बढ़ाने और लागू करने के साधन के रूप में माना जाता था। 1980 के दशक में जनहित याचिका की बारीकियों ने एक नया मोड़ लिया, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की अवधारणा स्थापित की। भारतीय न्यायपालिका ने अनेक नवीन उपायों के माध्यम से यह माना कि पारंपरिक मुकदमेबाजी प्रणाली, जो अत्यधिक व्यक्ति-केंद्रित और विरोधी थी, व्यक्तियों, विशेषकर कमजोर और वंचितों की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थी।
जनहित याचिका की अवधारणा के उद्भव के साथ, न्यायालय ने अपने व्यापक संवैधानिक अधिकार और अपने कुछ प्रमुख स्रोतों, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपयोग किया था। ऐसा एक ढांचा तैयार करने, व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करने तथा मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
जनहित याचिका के पूर्ववर्ती उदाहरणों में से एक हुसैनारा खातून एवं अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना (1979) का मामला है, जो बिहार में विचाराधीन कैदियों की भयानक स्थिति से संबंधित है। कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर करते हुए एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कई कैदियों को उनके कथित अपराधों के लिए निर्धारित सजा से अधिक अवधि तक जेल में रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ता की विश्वसनीयता को स्वीकार किया और तत्पश्चात निर्देश जारी करते हुए पुष्टि की कि ‘शीघ्र सुनवाई का अधिकार’ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के मूलभूत तत्वों में से एक है।
डॉ. उपेन्द्र बक्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1981) के एक अन्य मामले में, दो प्रमुख कानूनी विद्वानों ने सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं, जिनमें कानून के कई दुरुपयोगों पर प्रकाश डाला गया, और उन्होंने दावा किया कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं। उनकी चिंताओं में विभिन्न मुद्दे शामिल थे, जिनमें संरक्षण गृहों में अमानवीय स्थिति, अदालती कार्यवाही में होने वाली देरी, मानव तस्करी, समलैंगिक शोषण के लिए बच्चों का आयात, तथा बंधुआ मजदूरों को न दिए जाने वाले वेतन आदि शामिल थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुद्दों पर विचार करने के बाद, प्रभावित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया तथा दिशानिर्देश और आदेश जारी किए, जिनसे प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ था।
शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) के एक अन्य मामले में, बम्बई की पुलिस जेलों में बंद महिला कैदियों की दुर्दशा पर विचार किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि वे हिरासत में हिंसा की शिकार थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए बम्बई स्थित सामाजिक कार्य महाविद्यालय के निदेशक को बम्बई केंद्रीय जेल का दौरा करने का निर्देश दिया। निदेशक को कई महिला कैदियों से साक्षात्कार (इंटरव्यू) करने का निर्देश दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें यातना या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था, तथा अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। अपने निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि महिला कैदियों की देखभाल महिला कांस्टेबलों द्वारा की जानी चाहिए तथा महिला संदिग्धों से पूछताछ केवल महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
इसी प्रकार, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं अन्य (1984) के मामले में, बाल एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पारंपरिक न्यायिक तरीकों से हटकर अधिक समकालीन तरीकों की ओर जाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि ऐसे नवीन दृष्टिकोण विकसित किए जा सकें, जो व्यापक जनसंख्या के मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें और उन्हें बनाए रख सकें।
यद्यपि जनहित याचिका (पीआईएल) के दुरुपयोग को रोकना महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार द्वारा इसे विनियमित करने के प्रयासों से उन लोगों में भारी विरोध उत्पन्न हो सकता है, जिन्हें डर है कि ऐसे उपायों से उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में, सर्वोच्च न्यायालय को जनहित याचिका मामलों में स्थगन आदेशों और प्रतिषेधो के संबंध में सुरक्षा उपाय शामिल करके हस्तक्षेप करना चाहिए।
जनहित याचिका के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल की चिंताओं के बावजूद, यह सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, जो समाज के सभी वर्गों के कल्याण में सहायक है। इसके अलावा, यह न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में कार्य करता है। इसने सामाजिक अन्याय को दूर करने में खुद को लाभकारी साबित किया है और यह व्यक्ति-केंद्रित होने के बजाय हाशिए पर पड़े समुदायों की जरूरतों को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्थागत प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।
जनहित याचिका और रिट के बीच अंतर
| मापदंड | जनहित याचिका | रिट |
| अर्थ | जनहित याचिका एक कानूनी उपाय है जिसमें विभिन्न सामाजिक असमानताओं और संवैधानिक अधिकारों के हनन को संबोधित करने के लिए याचिका दायर की जाती है। | रिट भी कानूनी उपचार हैं जिनमें किसी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। |
| प्रक्रिया | जनहित याचिका के तहत याचिका दायर करने की प्रक्रिया कम प्रयास वाली और सस्ती है। | रिट के तहत याचिका दायर करने की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से अधिक महंगी, समय लेने वाली और अधिक कानूनी औपचारिकताएं वाली होती है। |
| लॉकस स्टैंडाई | जनहित याचिका के तहत, लॉकस स्टैंडाई को माफ किया जा सकता है। | रिट के तहत याचिका दायर करते समय, एक लॉकस स्टैंडाई होना चाहिए। |
| साक्ष्य | जनहित याचिका के तहत साक्ष्य जुटाने और उसकी जांच की सख्ती से जांच नहीं की जाती। | रिट कार्यवाही के अंतर्गत साक्ष्य की कठोरतापूर्वक एवं गहनता से जांच की जाती है। |
| निर्णय | जनहित याचिका के तहत मामलों में दिए गए निर्णय निर्णायक प्रकृति के होते हैं तथा भविष्य में मामलों के लिए रेशियो डिसिडेंडी बन सकते हैं। | रिट के तहत, हालांकि निर्णय ज्यादातर निजी हित के मामले से संबंधित होते हैं, वे कभी-कभी रेशियो डिसिडेंडी और ओबिटर डिक्टा का भी हिस्सा बन सकते हैं। |
| कानूनी समर्थन | जनहित याचिका के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का किसी भी कानून में उल्लेख नहीं है तथा इसे न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं द्वारा रिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। | भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति) और अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति) के तहत रिट का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। |
निष्कर्ष
भारतीय संविधान अपने भाग III के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। मैग्ना कार्टा से लेकर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तक इन अधिकारों का ऐतिहासिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की दिशा में एक वैश्विक क्रांति को प्रदर्शित करता है। भारतीय संविधान न केवल इन अधिकारों को स्पष्ट करता है, बल्कि इनके प्रवर्तन के लिए तंत्र भी प्रदान करता है, जिसमें अनुच्छेद 32 इस सुरक्षात्मक ढांचे की नींव के रूप में कार्य करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेषाधिकार रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मौलिक अधिकार केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि उनके उल्लंघन से सक्रिय रूप से संरक्षित हैं। अनुच्छेद 226 के साथ यह प्रावधान न्यायिक समीक्षा और उपचार के दायरे को व्यापक बनाता है तथा कानून के शासन को मजबूत करता है।
संवैधानिक उपचार जनहित याचिका की अवधारणा का अनुसरण करते हैं, जो व्यक्ति-केंद्रित समाधान के बजाय सामूहिक उपचार की ओर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जनहित याचिका का महत्व पारंपरिक व्यक्ति-केंद्रित मुकदमेबाजी से एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण की ओर गतिशील बदलाव को रेखांकित करता है जो सामूहिक शिकायतों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों की शिकायतों को संबोधित करता है।
ऐतिहासिक मामलों ने जनहित याचिकाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाया है, जिससे उनकी न्यायिक जवाबदेही बढ़ी है और सामाजिक कल्याण पर ध्यान दिया गया है। अंततः, संवैधानिक संरचना और न्यायिक व्याख्याएं सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक नैतिकता को कायम रखती हैं तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि मौलिक अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों के लिए जीवंत वास्तविकता बने रहें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों द्वारा रिट जारी की जा सकती है?
हां, किसी भी प्रकार की रिट भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है।
क्या रिट में शिकायत शामिल होती है?
रिट में एक याचिका होती है।
सामान्यतः किस प्रकार की रिट का प्रयोग किया जाता है?
परमादेश सर्वाधिक प्रचलित रिटों में से एक है, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, न्यायाधिकरण या निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किए बिना अपने कार्यों का निर्वहन करने का आदेश देता है।
क्या जनहित याचिका और रिट समान हैं?
जनहित याचिका संवैधानिक उपचार प्रदान करने की एक अवधारणा या कार्यान्वयन की एक विधि है, जबकि रिट ऐसे कार्यान्वयन का माध्यम है। दोनों ही संवैधानिक उपचारों के आयाम से संबंधित हैं।
संदर्भ