यह लेख Arya Senapati द्वारा लिखा गया है । यह सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984) के मामले का विश्लेषण उसके तथ्यात्मक मैट्रिक्स, कानूनी मुद्दों, शामिल कानूनी प्रावधानों और दिए गए अंतिम निर्णय के माध्यम से करने का प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना (रेस्टिट्यूशन) की वैधता से संबंधित है और यह अपनी प्रकृति में एक वैवाहिक मामला है। लेख अन्य कानूनों से भी संबंधित है जो या तो मामले द्वारा समर्थित या खारिज किए गए हैं। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसे समाज, पारिवारिक संरचना, जाति और परंपराओं की निरंतरता के निर्माण का अभिन्न अंग माना जाता है। एक मिलनसार प्राणी के रूप में, मनुष्य को संगति (कंपेनियन) की आवश्यकता होती है जिसे विवाह की संस्था पूरी करती है। जबकि विभिन्न परंपराएँ और संस्कृतियाँ विवाह के विचार और संस्था को अलग-अलग तरीके से देखती हैं, यह अपने दीर्घकालिक उद्देश्य और लोकाचार (इथोस) के कारण उन सभी में प्रासंगिक (रिलेवेंट) है। विशेष रूप से हिंदू समाज में, विवाह को एक संस्कार और दो व्यक्तियों के बीच एक पवित्र मिलन माना जाता है जिसे इसकी वैधता को मूर्त रूप देने के लिए औपचारिक संस्कारों और प्रथाओं के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। प्रथागत हिंदू कानून विवाह को एक स्थायी मिलन मानता था और अलगाव (सेपरेशन) या तलाक की अवधारणा की परिकल्पना नहीं करता था। हिंदू विवाह की परंपरा के तहत जो विचार समाहित था वह यह था कि बंधन जीवन भर के लिए शाश्वत रहता है और इसे इच्छाशक्ति से नहीं तोड़ा जा सकता।
समय बीतने और आधुनिक विचारों, नारीवादी आंदोलनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शक्तिहीनता की मान्यता के साथ, विवाह के अपूरणीय टूटने से निपटने के उपाय के रूप में तलाक की शुरुआत की गई। कई आधारों को मान्यता दी गई थी जिसके आधार पर एक पति या पत्नी दूसरे को तलाक दे सकता था। समाज में पितृसत्तात्मक (पेट्रियार्कल) संरचनाओं के अस्तित्व के कारण घरेलू हिंसा और क्रूरता में वृद्धि के साथ, विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि इसके भीतर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
तलाक कई महिलाओं के हाथों में एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण बन गया, जो खुद को एक क्रूर और असंगत रिश्ते की सीमाओं से मुक्त करना चाहती थीं। जबकि राज्य द्वारा व्यक्तिगत कानूनों के क्षेत्र में बहुत अधिक हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना जाता है, सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा करना और उसके भीतर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य है। इन अतिव्यापी (ओवरलैपिंग) कर्तव्यों को संतुलित करने के लिए, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की अवधारणा को मान्यता दी गई थी। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के पीछे मुख्य विचार पति-पत्नी को एक निश्चित समय के लिए एक साथ रहने या सहवास (कोहेबिट) करने की अनुमति देना था ताकि यह पूरी तरह से पता लगाया जा सके कि वे अपने वैवाहिक संबंधों को समाप्त करना चाहते हैं या सुलह की कोई गुंजाइश है। यदि न्यायालय सुलह की गुंजाइश देखता है, तो वह अनिश्चित काल के लिए विवाह को टूटने से बचाने की कोशिश करेगा।

जहाँ एक विचारधारा ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और इसे विवाह संस्था की रक्षा के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में देखा, वहीं दूसरी ओर विरोधी धारा ने इसे महिलाओं की निजी गोपनीयता और स्वतंत्रता के साथ-साथ उनकी स्वतंत्र इच्छा का राज्य प्रायोजित उल्लंघन माना। विभिन्न तर्कों के आधार पर, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की संवैधानिकता के बारे में कई निर्णय किए गए, जिनमें से सबसे प्रमुख श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984) का मामला है , जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह संस्था और इसकी पवित्रता को संरक्षित करने के उपाय के रूप में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
मामले का विवरण
अपीलकर्ता: श्रीमती सरोज रानी
प्रतिवादी: सुदर्शन कुमार चड्ढा
न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
बेंच: सब्यसाची मुखर्जी, सैयद मुर्तज़ा फ़ज़लाली
दिनांक: 08.08.1984
उद्धरण: 1984 एआईआर 1562
मामले के तथ्य
इस मामले में पक्षकार पति-पत्नी हैं, जिनका विवाह 24 जनवरी, 1975 को हिंदू वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार जालंधर शहर में हुआ था। उनकी पहली लड़की का जन्म 4 जनवरी, 1976 को हुआ और उसका नाम मेनका रखा गया। उनकी दूसरी बेटी गुड्डी का जन्म 28 फरवरी, 1977 को हुआ। 16 मई, 1977 को वे अंतिम बार एक साथ रहे। उस दिन, पति, जो मामले में प्रतिवादी है, ने पत्नी, अपीलकर्ता को अपने घर से निकाल दिया और खुद भी उसके समाज से अलग हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में, उनकी दूसरी बेटी की 6 अगस्त, 1977 को प्रतिवादी के घर पर मृत्यु हो गई। 17 अक्टूबर, 1977 को पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के दावों के साथ पति पर मुकदमा दायर किया।
याचिका में अपीलकर्ता ने दावा किया कि उनकी शादी का इतिहास कठिन और उथल-पुथल भरा रहा है। उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार के कई उदाहरण हैं। इन उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद, उसने अदालत के आदेश के माध्यम से वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की राहत के लिए प्रार्थना की। 21 मार्च, 1978 की तारीख को, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी ने एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ता को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रति माह 185 रुपये भरण-पोषण और मुकदमे के खर्च के रूप में 300 रुपये दिए गए। 28 मार्च, 1978 को, उप-न्यायाधीश द्वारा एक सहमति डिक्री पारित की गई, जिसमें वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना को मंजूरी दी गई।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी ने दुर्व्यवहार के किसी भी मामले से इनकार नहीं किया और इस तथ्य से इनकार किया कि उसने अपीलकर्ता को अपने घर से निकाल दिया था या खुद को उसके समाज से अलग कर लिया था या उसके लिए उसके मन में कोई प्यार और स्नेह नहीं था। इन आधारों पर, वह वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना पर सहमति डिक्री से सहमत हो गया। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि वह प्रतिवादी के घर गई थी और डिक्री पारित होने के बाद दो दिनों तक उसके साथ रही। इस तथ्य को किसी भी अदालत ने स्वीकार नहीं किया और सभी अदालतें इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना देने वाली सहमति डिक्री पारित होने के बाद कोई सहवास नहीं हुआ है। इस तथ्य को सर्वोच्च न्यायालय के सामने चुनौती नहीं दी गई।
19 अप्रैल, 1979 को प्रतिवादी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री पारित होने के बाद से एक वर्ष बीत चुका है और कोई सहवास नहीं हुआ है और इसलिए उस आधार पर उसे तलाक की डिक्री प्रदान की जाना चाहिए। अपीलकर्ता ने कहा कि उसके माता-पिता उसे सहमति डिक्री के एक महीने बाद प्रतिवादी के घर ले गए लेकिन प्रतिवादी ने उसे दो दिनों तक अपने घर में रखा और उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया। अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 28A के तहत एक आवेदन भी दायर किया जिसमें कहा गया कि उसके पति को उप-न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री का पालन करना चाहिए और डिक्री के अनुसार सहवास स्थापित करना चाहिए। यह आवेदन उप-न्यायाधीश के समक्ष लंबित था जब प्रतिवादी द्वारा तलाक की याचिका दायर की गई थी।
जिला न्यायालय का निर्णय
जिला न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा दायर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने दो कानूनी मुद्दे तय किए। पहला यह था कि क्या उप-न्यायाधीश द्वारा पारित सहमति डिक्री के बाद वैवाहिक अधिकारों की कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई है और दूसरा यह था कि पति कानून के अनुसार किस राहत का हकदार है। पक्षों के साथ लंबित सभी सिविल और आपराधिक मामलों के सभी साक्ष्यों पर गहन विचार करने के बाद, जिला न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 28 मार्च, 1978 या जिस तारीख को सहमति डिक्री प्राप्त हुई थी, उसके बाद पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों या सहवास की कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई है। जिला न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। प्रतिवादी को मिलने वाली राहत के बारे में बात करते हुए, न्यायालय ने देखा कि चूंकि डिक्री सहमति से हुई थी और उस अवधि के दौरान, आपसी सहमति से तलाक देने के लिए धारा 13B जैसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं था, इसलिए प्रतिवादी तलाक की डिक्री का हकदार नहीं था।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय
जिला न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर की। पत्नी ने तर्क दिया कि पति अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता, जो गलती उसके साथ सहवास करने से इनकार करने से की है। उच्च न्यायालय ने धर्मेंद्र कुमार बनाम उषा कुमारी (1977) के मामले के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि अपीलकर्ता को अपने विवाद में इस मामले का हवाला देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि पति अपनी गलतियों या भूल का कोई लाभ नहीं उठा रहा था। संदर्भित मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यह मानना उचित नहीं होगा कि जिस पक्ष के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, उसे जो राहत या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का हक है, वह राहत उस व्यक्ति को देने से मना कर दिया जाना चाहिए जो उसके विरुद्ध पारित डिक्री का अनुपालन नहीं करता है। उच्च न्यायालय के अनुसार, धारा 23 (1) (a) के अर्थ में किसी पक्ष को गलत होने के लिए, जिस आचरण का आरोप लगाया गया है, वह पुनर्मिलन (रियूनियन) प्रस्ताव के मात्र इनकार से अधिक गंभीर होना चाहिए। यह इतना गंभीर कदाचार होना चाहिए कि पक्षकारों को राहत न देने का बचाव किया जा सके।
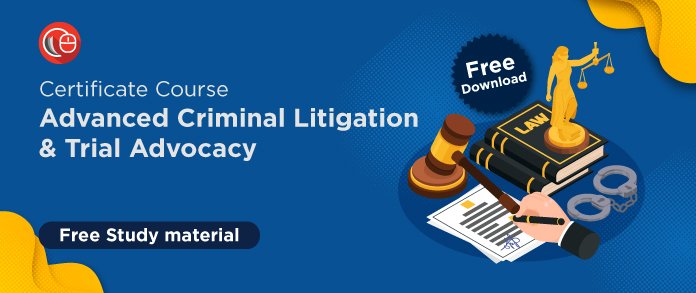
इस संदर्भ के आधार पर, उच्च न्यायालय ने पत्नी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पति अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता। उच्च न्यायालय ने माना कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश अपने वास्तविक स्वरूप में सहमति का आदेश नहीं था, बल्कि यह एक मिलीभगत वाला आदेश था और इसलिए यह पति को तलाक के आदेश के लिए अयोग्य बनाता है। इस मामले से निपटने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने महसूस किया कि इस मुद्दे पर अधिक ध्यान और विचार-विमर्श की आवश्यकता है और इसलिए, उन्होंने मामले को मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित (रैफर) किया और मामले पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ (डिवीजन बेंच) के गठन की मांग की।
इसके बाद मामला खंडपीठ के पास चला गया और मुख्य न्यायाधीश संधावालिया ने कानून के विभिन्न प्राधिकारों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि सहमति की डिक्री को वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री को प्राप्त करने से पति को वंचित करने के लिए कपटपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। खंडपीठ ने गौर किया कि खंडपीठ के समक्ष पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने विचारण न्यायालय के तथ्यात्मक निष्कर्षों का कोई संदर्भ नहीं दिया और इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि डिक्री पारित होने के बाद वैवाहिक अधिकारों की कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई थी। वकील ने इस बचाव पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया कि पति को अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसने सहमति डिक्री के निष्पादन के माध्यम से सहवास करने से इनकार कर दिया था। वकील ने केवल इस आधार पर भरोसा किया कि डिक्री एक कपटपूर्ण थी। जोगिंदर सिंह बनाम श्रीमती पुष्पा (1968) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि सभी मामलों में सहमति की डिक्री को कपटपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, और ऐसे मामलों में जहां पक्षों ने विवाद को निपटाने के विभिन्न प्रयासों के बाद डिक्री के आवेग पर सहमति व्यक्त की थी, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पति को डिक्री प्राप्त करने से वंचित नहीं करती है। धारा 23 में केवल यह कहा गया है कि जब भी न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा प्रदान की गई किसी भी राहत को देने का प्रयास करता है, तो राहत देने वाली डिक्री पारित करने से पहले जहां भी व्यावहारिक रूप से संभव हो, पक्षों के बीच सुलह तक पहुंचने का प्रयास करना उसका कर्तव्य है। इन सभी पहलुओं के आधार पर उच्च न्यायालय ने माना कि डिक्री को कपटपूर्ण मानना संभव नहीं है और पति को राहत देने वाली डिक्री से वंचित नहीं किया जा सकता है।
शामिल कानूनी मुद्दे
इस वैवाहिक विवाद पर निर्णय लेते समय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ प्राथमिक लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर विचार किया। वे हैं:
- क्या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9, जो वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है ?
- क्या प्रतिवादी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना प्रदान करने वाली सहमति डिक्री का अनुपालन करने में विफल रहने के बाद भी तलाक की डिक्री का हकदार है?
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 को समझना
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की अवधारणा से संबंधित है। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के पीछे सिद्धांत यह है कि जब भी दो पक्षों के बीच कोई विवाद होता है, तो उनमें से कोई भी उपाय के रूप में पुनर्स्थापना की मांग कर सकता है। इस उपाय में, पति-पत्नी को एक-दूसरे के साथ सहवास फिर से शुरू करने और यह आकलन करने के लिए कहा जाता है कि क्या वे अपने मतभेदों को सुलझा सकते हैं और अपने वैवाहिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण (कोर्डियली) ढंग से बनाए रखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जब भी कोई साथी स्वेच्छा से या बलपूर्वक दूसरे के साझा (शेयर्ड) घर या समाज से अलग हो जाता है, तो यह उपाय लागू होता है। न्यायालय वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश देता है और भागीदारों को एक-दूसरे के साथ सहवास करने का आदेश देता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विवाह की पवित्रता को बनाए रखना और संरक्षित करना है क्योंकि इसे भारतीय परंपराओं में एक संस्कार माना जाता है।
श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन चड्ढा (1984) के मामले में , विवाह को पति और पत्नी के बीच एक मिलन के रूप में परिभाषित किया गया था, जो एक समान जीवन जीते हैं और एक-दूसरे के सामाजिक परिवेश और गतिविधियों में भाग लेते हैं, खुशियाँ साझा करते हैं और मुसीबत के क्षणों में एक-दूसरे का साथ देते हैं। यौन संबंधों को भी वैवाहिक संबंधों के एक पहलू के रूप में देखा गया है, भले ही यह विवाह का प्राथमिक घटक न हो, जिसे न्यायालय साथी की इच्छा के बिना भी पुनर्स्थापित कर सकता है। इसके विपरीत, धारा 9 के आवेदन के माध्यम से, न्यायालय परित्यक्त (अबॉन्डेंड) जीवनसाथी के लिए राहत के रूप में सामान्य जीवन, घर और समाज की पुनर्स्थापना को लागू कर सकता है।
धारा 9 में प्रावधान है कि ऐसी परिस्थिति में जब पति या पत्नी बिना किसी उचित आधार, कारण या स्पष्टीकरण के दूसरे के साथ रहने से पीछे हट जाते हैं, तो दूसरा पति या पत्नी जिला न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और अपने वैवाहिक संबंध को बनाए रखने के लिए वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय मांग सकता है। एक बार जब न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट हो जाता है कि परित्याग करने वाले पति या पत्नी के पास उसके पति या पत्नी के साथ न रह कर खुद को अलग करने का कोई उचित आधार नहीं है, तो वह वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दे सकता है।
प्रावधान के अनुसार, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के आदेश को मंजूरी देने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
- दोनों में से किसी भी पक्ष ने बिना किसी उचित कारण/आधार या स्पष्टीकरण के अपने पति या पत्नी के जीवन और समाज से स्वयं को अलग कर लिया है।
- न्यायालय का मानना है कि याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा दिए गए बयान सत्य एवं पुष्ट हैं।
- पुनर्स्थापना की याचिका को अस्वीकार करने तथा याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करने का कोई कानूनी आधार मौजूद नहीं है।
समाज शब्द का अर्थ सहवास और संगति माना जाता है, जो आमतौर पर वैवाहिक संबंधों से अपेक्षित होता है। इसलिए समाज से अलग होने को वैवाहिक संबंधों से अलग होने के रूप में समझा जाता है।

श्रीमती मंजुला झवेरीलाल बनाम झवेरीलाल विट्ठल दास (1973) के मामले में , न्यायालय ने माना कि जब भी कोई पीड़ित पक्ष वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना करते हुए याचिका दायर करता है और पर्याप्त रूप से यह दर्शाता है कि प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के पीड़ित पक्ष की संगति से खुद को अलग कर लिया था, तो न्यायालय वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का अनुतोष प्रदान कर सकता है।
अपीलकर्ता के तर्क
अपीलकर्ता (पत्नी) के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी (पति) ने पुनर्स्थापना डिक्री मांगने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ रहने का इरादा नहीं किया। पुनर्स्थापना के लिए सहमति डिक्री प्राप्त करने के बाद भी, पति ने अपीलकर्ता के साथ सहवास से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने डिक्री का पालन किया था और उसके साथ रहने चली गई थी लेकिन दो दिनों के बाद उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। इसलिए, पति को तलाक की डिक्री नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसे अपनी गलतियों का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी मुकदमे के शुरुआती चरण से ही तलाक चाहता था और सहमति डिक्री केवल मामले को अपने पक्ष में हेरफेर करने के लिए एक रणनीतिक कदम था।
प्रतिवादी के तर्क
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि सहमति डिक्री पारित होने के बाद भी अपीलकर्ता ने उसके साथ सहवास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता का यह कथन कि उसने सहवास फिर से शुरू करने का प्रयास किया और दो दिनों तक उसके साथ रही जिसके बाद उसे बाहर निकाल दिया गया, एक मनगढ़ंत और झूठा कथन है। अपीलकर्ता के कृत्य से उसे बहुत ठेस पहुंची है। सहमति डिक्री मिलीभगत वाली प्रकृति की नहीं थी और इसलिए उनकी शादी के अपूरणीय टूटने के कारण उसे तलाक दिया जाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अभिलेखों (रिकॉर्ड) पर मौजूद तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि यह डिक्री कपटपूर्ण नहीं थी और पक्षों के बीच कोई गुप्त समझौता नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पत्नी ने पति के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे, जिसका उसने खंडन किया था और उसने कहा था कि वह उसे वापस लेने और उसके साथ रहने के लिए सहमत है। इन तथ्यों के आधार पर सहमति डिक्री पारित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, पक्षों के बीच किसी भी तरह की कपटपूर्णता पाना असंभव था और वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के बहुमत के फैसले से सहमत था कि जोगिंदर सिंह बनाम श्रीमती पुष्पा (1968) के मामले के अनुसार , सभी सहमति डिक्री प्रकृति में कपटपूर्ण नहीं होती हैं। खासकर जब वैवाहिक विवादों की बात आती है, तो सहमति डिक्री को कपटपूर्ण नहीं माना जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के पीछे विधायी मंशा से यह स्पष्ट है कि आपसी सहमति से तलाक जैसी अवधारणाएं भारत में तलाक कानून की व्यवस्था से अलग नहीं हैं, लेकिन चूंकि यह मामला इस प्रावधान की शुरूआत से पहले आया था, इसलिए इसे इस मामले में लागू नहीं किया जा सका। इन टिप्पणियों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के बहुमत के दृष्टिकोण को कानूनी मुद्दे पर स्वीकार कर लिया कि क्या यह डिक्री मिलीभगत वाली थी या नहीं।
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ता-पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने खंडपीठ के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी, जिसने माना कि सहमति डिक्री को कानून में प्रमाणित किया जा सकता है क्योंकि यह प्रकृति में कपटपूर्ण नहीं थी। इसके बजाय, वकील ने यह आग्रह करने की कोशिश की कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23(1)(a) में उल्लिखित “गलत” अभिव्यक्ति जो किसी पक्ष को अपने स्वयं के गलत होने का लाभ उठाने से रोकती है, पति को तलाक की डिक्री से वंचित करती है। वकील ने तर्क दिया कि पति-प्रतिवादी शुरू से ही अपने पक्ष में तलाक की डिक्री चाहता था। इस इच्छा के आधार पर, उसने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री के पारित होने पर आपत्ति नहीं की। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पति वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री पर सहमत हो गया क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि वह अंततः तलाक की डिक्री चाहता है। वह जानता था कि वह डिक्री का सम्मान नहीं करने वाला था। यह तर्क दिया गया कि उनका इरादा अदालत और अपीलकर्ता को गुमराह करने का था और फिर उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से इनकार कर दिया और इसलिए उन्हें अपनी गलतियों का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता की दलीलों में इन आरोपों का कोई उल्लेख नहीं है। जब सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस कमी की ओर ध्यान दिलाया, तो वकील ने अपनी दलील में संशोधन करने का अवसर देने की प्रार्थना की और कहा कि वकील की गलती के कारण पक्षों को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐसे तथ्य देखे हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले, जिन तर्कों पर ज़ोर दिया गया, उन पर कोई दलील नहीं दी गई। दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसी अन्य न्यायालय में तर्क नहीं दिया गया। तीसरे, जो तथ्य पेश किए गए और जो आरोप पत्नी ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंडपीठ में लगाए, वे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगाए गए आरोपों के विरोधाभासी थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने अपना पूरा मामला इस तथ्य पर बनाया कि वह और उसका पति वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए सहमति डिक्री पारित होने के बाद ही दो दिनों के लिए सहवास में आए थे। तब पत्नी द्वारा जो आधार दिया गया था वह यह था कि पति ने पत्नी को फंसाकर और उसके साथ सहवास न करके न्यायिक पृथक्करण (सेपरेशन) की डिक्री प्राप्त करने की कोशिश की ताकि तलाक की डिक्री प्राप्त की जा सके। पत्नी के मामले में उत्पन्न होने वाले ये विरोधाभास उसके तर्कों को कमजोर और निराधार बनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, मामले के इस चरण में दलीलों को संशोधित करने के लिए समय देने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि इससे उसे मामले से असंगत तथ्य प्रस्तुत करने का मौका मिल जाता।
अपीलकर्ता के वकील ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह “अपनी गलती का फ़ायदा उठाना” वाक्यांश की इस तरह से व्याख्या करे कि यह चालाक पतियों को भारतीय पत्नियों को धोखा देने और उन्हें उनके बेईमान पतियों के कहने पर पीड़ित होने से रोक सके। इस वृद्धि के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि इस मामले में इस तरह की व्याख्या के तथ्यात्मक अनुप्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है और इस तरह की व्याख्या के लिए विधायी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होगी जो न्यायालय की शक्तियों के भीतर नहीं है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी भी मानसिक पीड़ा की अनुपस्थिति में और ऐसी स्थिति की उपस्थिति में जो दर्शाती है कि विवाह टूट गया है और पक्ष अब पति-पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो उस संबंध को समाप्त करना बेहतर है।
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान टी. सरिता बनाम वेंकट सुब्बैया (1983) के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया गया , जिसमें न्यायाधीश ने कहा था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में दो पति-पत्नी के बीच दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय एक असभ्य और बर्बर उपाय है, जो निजता और मानव सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होता है।
विद्वान एकल न्यायाधीश ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित धारा 9 को संवैधानिक रूप से शून्य घोषित किया क्योंकि यह संवैधानिक कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार शून्य घोषित किया जाएगा। विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और इसकी नकारात्मक व्याख्या में कहा गया है कि कोई भी राज्य प्राधिकरण कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकता है। यह मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि जब भी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इसका परिणाम निजता के व्यक्तिगत अधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन होता है क्योंकि एक महिला को उसकी स्वतंत्र इच्छा से वंचित किया जाता है कि उसका शरीर कब और कैसे किसी अन्य मानव के प्रजनन (प्रोक्रिएशन) का वाहन माना जाता है।
विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश एक महिला को उसकी पसंद और अंतरंग (इंटिमेट) निर्णयों पर शारीरिक स्वायत्तता से वंचित करता है। विद्वान न्यायाधीश के अनुसार, एक महिला जो स्थायी या अस्थायी वैवाहिक दरार के कारण अपने पति से दूर रहना चाहती है, उसे उसके पति के साथ रहने और उसके इनकार के बावजूद उसके पति के साथ बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। उस पर ऐसे समय में लागू किया गया ऐसा उपाय, जब वह तलाक लेने पर विचार कर रही है, उसकी मानसिक, शारीरिक और जीवन की स्थिति को जटिल बनाता है और आजीवन आघात देता है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि प्रावधान किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है जो वैध है और प्रावधान से उत्पन्न होने वाली सामान्य भलाई की कोई अवधारणा नहीं है। इसलिए, प्रावधान सामाजिक भलाई के अधीन नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार यह प्रावधान मनमाना और भेदभावपूर्ण माना गया, जो समानता के अधिकार से संबंधित है। विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों के अनुसार, प्रावधान ने उचित वर्गीकरण के परीक्षण का उल्लंघन किया क्योंकि इसने पति और पत्नी के बीच कोई अंतर नहीं किया क्योंकि इसने दोनों को उपाय उपलब्ध कराया लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि असमान वास्तविकता के बावजूद उपचार की समानता न्याय या संवैधानिकता के सिद्धांतों के लिए आदर्श नहीं है। विद्वान न्यायाधीश ने यह भी देखा कि कैसे वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का उपाय मुख्य रूप से पति द्वारा मांगा गया था न कि पत्नी द्वारा।
विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियां हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह चौधरी (1983) के निर्णय में असहमतिपूर्ण थीं, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया था। निर्णय में, विद्वान न्यायाधीश ने माना कि धारा 9 के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्स्थापन डिक्री का उद्देश्य अलग-अलग पक्षों के बीच सहवास को बढ़ावा देना था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे संभवतः एक साझा घर में वैवाहिक सद्भाव में एक साथ रह सकते हैं। प्रावधान के पीछे प्राथमिक विचार विवाह संस्था को संरक्षित करना है। यौन संभोग केवल उन चीजों में से एक है जो सहवास में शामिल हैं। इसे सहवास का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र चीज के बराबर नहीं माना जा सकता है। न्यायालय पति-पत्नी के बीच यौन संभोग को लागू नहीं कर सकते और न ही करते हैं। वैवाहिक संबंधों में बहुत सी चीजें शामिल होती हैं जिनमें यौन संबंध केवल एक समान है। यह बल्कि अवास्तविक और तुच्छ प्रकृति का है। उपाय वैवाहिक सौहार्द की ओर लक्षित है न कि यौन संभोग की ओर। वैवाहिक सहवास को यौन संभोग के बराबर मानना तथा वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना को वैवाहिक गोपनीयता पर सरकार द्वारा अधिकृत आक्रमण मानना कानूनी भ्रांति (इंवेशन) है।
दोनों निर्णयों का अवलोकन करने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को अपनाया। वैवाहिक का तात्पर्य केवल विवाह से संबंधित किसी भी चीज से है तथा पति-पत्नी के बीच साझा किए गए संबंधों से है। वैवाहिक अधिकारों में पति-पत्नी के एक-दूसरे के समाज का हिस्सा होने का अधिकार निहित है। यह विवाह संस्था का एक अंतर्निहित पहलू है। धारा 9 में इस धारा के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 9 केवल उस कानून का संहिताकरण है जो इससे बहुत पहले अस्तित्व में था। यह कानून सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 21 नियम 32 था जो वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना या इसके लिए निषेधाज्ञा (इंजक्शन) के विशिष्ट प्रदर्शन से संबंधित था। इसमें कहा गया है कि जब भी कोई पक्ष जिसके विरुद्ध किसी अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना या निषेधाज्ञा के लिए डिक्री पारित की जाती है और पक्ष के पास डिक्री का पालन करने का विकल्प होता है, लेकिन वह जानबूझकर इससे बचता है, तो डिक्री को संपत्ति की कुर्की (अटैचमेंट) द्वारा लागू किया जा सकता है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि, अनुबंध के शांतिपूर्ण निष्पादन के लिए डिक्री के विपरीत, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दंडात्मकता न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है, जहां इस तरह के डिक्री के प्रति जानबूझकर अवज्ञा होती है। ऐसे मामलों में, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री को निष्पादित करने के लिए उनकी संपत्तियां कुर्क की जा सकती हैं। यह वित्तीय मंजूरी का एक रूप है जिसे न्यायालयों द्वारा लगाया जाता है। इसे सामाजिक उद्देश्य के रूप में विवाह की पवित्रता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के दृष्टिकोण के खिलाफ खड़ा हुआ और वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में प्रावधानों के गठन को बरकरार रखा।
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के गीता लक्ष्मी बनाम जीवीआरके सर्वेश्वर राव (1982) नामक एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया , जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने माना था कि पति द्वारा स्वीकार किया गया कदाचार केवल वैवाहिक पलायन की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री की अवज्ञा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार करना और उसे घर से निकाल देना भी शामिल है। इस तर्क के आधार पर, न्यायालय ने पति को धारा 13(1A) के तहत तलाक के लिए डिक्री देने से मना कर दिया था। इस मामले के तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले से बहुत अलग थे और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने मिसाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वर्तमान मामले में पति द्वारा दुर्व्यवहार या पत्नी को घर से निकालने का कोई आरोप या सबूत नहीं था।
इन सभी कारकों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः निर्णय लिया कि पति तलाक की डिक्री का हकदार है, लेकिन यह देखते हुए कि एक भारतीय तलाकशुदा पत्नी हमेशा भौतिक रूप से वंचित होती है, पति को तलाक की अंतिम डिक्री दिए जाने के बाद पत्नी को तब तक भरण-पोषण देने का आदेश दिया जाना चाहिए जब तक कि पत्नी दोबारा शादी न कर ले और पति का यह भी कर्तव्य है कि वह विवाह से अपनी एकमात्र जीवित बेटी का भरण-पोषण करे। पत्नी और बेटी को अलग-अलग भरण-पोषण दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने अपीलकर्ता पर इस अपील की लागत भी लगाई। इस प्रकार अपील खारिज कर दी गई।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत कौन याचिका दायर कर सकता है?
पति-पत्नी में से किसी को भी इस प्रावधान के तहत याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है। पति-पत्नी में से कोई भी व्यक्ति जो अपने पति-पत्नी द्वारा बिना किसी उचित या वाजिब कारण के अपने समाज से अलग होने से दुखी है, अपने वैवाहिक संबंधों और सहवास को बहाल या पुनर्स्थापना के लिए मजबूर करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। याचिका आम तौर पर एक पारिवारिक न्यायालय में दायर की जाती है, जिसका अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र पर होता है जहाँ विवाह संपन्न हुआ था, या जहाँ पति-पत्नी साथ रहते थे, या जहाँ पति-पत्नी ने खुद को अलग कर लिया है, वर्तमान में रह रहे हैं। पारिवारिक न्यायालय दोनों पक्षों को अपना मामला पेश करने का अवसर देता है। पीड़ित पक्ष को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी पति-पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के अपने समाज से अलग होने का फैसला किया और प्रतिवादी पति-पत्नी को कोई उचित कारण साबित करना होगा जिसके कारण वह समाज से अलग हुआ। कुछ उचित कारण क्रूरता, घरेलू हिंसा, मानसिक या शारीरिक दुर्व्यवहार आदि हो सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दे सकता है और परित्यक्त पति-पत्नी को परित्यक्त पति-पत्नी के साथ सहवास फिर से शुरू करने के लिए मजबूर कर सकता है।
डिक्री के निष्पादन का तरीका
दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 32 के माध्यम से निष्पादित किया जाता है । प्रावधान में कहा गया है कि जब भी किसी व्यक्ति पर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री लगाई जाती है और वह व्यक्ति जानबूझकर ऐसी डिक्री की अवहेलना करता है, तो उसकी संपत्ति को कुर्क करके इसे निष्पादित किया जा सकता है। यदि ऐसी संपत्ति छह महीने तक कुर्क रहती है और फिर भी निर्णीत-ऋणी ने डिक्री का पालन नहीं किया है, तो डिक्री-धारक संपत्ति को बेचने के लिए आवेदन कर सकता है और उस स्थिति में, न्यायालय ऐसी संपत्ति की बिक्री की व्यवस्था कर सकता है और इससे होने वाली कोई भी आय न्यायसंगत मुआवजे के रूप में डिक्री धारक को दी जा सकती है। शेष हिस्सा निर्णीत ऋणी को दिया जा सकता है।
पुनर्स्थापन हेतु याचिका की अस्वीकृति
सुशीला बाई बनाम प्रेम नारायण (1986) के मामले में , न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका के लिए बचाव के वैध आधारों का संदर्भ दिया, जिन्हें इसे अस्वीकार करने का दावा करने के लिए साबित किया जा सकता है। वे हैं:
- प्रतिवादी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के मुकदमे के विरुद्ध किसी अन्य वैवाहिक राहत का दावा करके बचाव कर सकता है
- प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दुर्व्यवहार का साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकता है, जिसके कारण उनके रिश्ते में खटास आई और उसे अपने पति/पत्नी को छोड़ना पड़ा।
- ऐसी परिस्थिति, जहां दोनों पति-पत्नी का एक साथ रहना संभव न हो, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु याचिका के विरुद्ध भी एक वैध बचाव है।
अस्वीकृति के कुछ आधार हो सकते हैं:
- याचिकाकर्ता या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की क्रूरता (मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, यौन)
- याचिकाकर्ता की ओर से वैवाहिक कदाचार जिसके कारण प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के साथ रहने में समस्या हुई होगी
- पति या पत्नी में से किसी एक का पुनर्विवाह या द्विविवाह
श्रीमती अरुणा गॉर्डन बनाम श्री जी.वी. गॉर्डन (1999) के मामले में, सबूत के भार के संदर्भ में , यह माना गया कि शुरू में, यह साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर रहता है कि प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण या आधार के अपने समाज से खुद को अलग कर लिया। फिर सबूत का भार प्रतिवादी पर आ जाता है कि वह साबित करे कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान गलत हैं या यह दिखाए कि उसके पास इस तरह के वापसी के लिए उचित आधार थे।
वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना पर ऐतिहासिक निर्णय
इस मामले पर न्यायिक निर्णय सिद्धांतों और व्याख्याओं का एक निशान छोड़ते हैं। सरोज रानी बनाम सुदर्शन चड्ढा (1984) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 9 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन ऐसे कई अन्य मामले भी हैं जहां प्रावधानों की उचित व्याख्या की गई है।
श्रीमती सुशीला बाई बनाम प्रेम नारायण राय (1985)
तथ्य
यह मामला अपीलकर्ता (पत्नी) द्वारा ग्वालियर के जिला न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन दायर करने से शुरू होता है जिसमें उसने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के आदेश के लिए प्रार्थना की। आवेदन में कहा गया कि उसका विवाह प्रतिवादी से 28 जून 1972 को हुआ था और विवाह के बाद वे साथ रहने लगे। साथ रहने के दौरान उसे कई बार दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और प्रतिवादी द्वारा उस पर हमला किया गया। ऐसी परेशानी भरी स्थिति के बाद भी उसने साथ रहना जारी रखा, फिर भी 1 मई 1977 को प्रतिवादी ने उसे उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक वह न कहे, उसे उसके पास वापस नहीं भेजा जाएगा। उसके माता-पिता ने प्रतिवादी को अपीलकर्ता को वापस लेने के लिए कई पत्र भेजे लेकिन उनका उत्तर नहीं दिया गया।
साक्ष्यों को देखने के बाद जिला न्यायालय ने पाया कि मुख्य मुद्दा यह है कि पत्नी अपने पति के साथ भोपाल में रहना चाहती है, जहां वह सरकारी कर्मचारी के रूप में तैनात है, लेकिन पति चाहता है कि पत्नी उसके पिता, माता और बहन के साथ रहे। अपीलकर्ता किसी भी अन्य पत्नी की तरह अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसके साथ वैवाहिक सुख का अनुभव करना चाहती है, लेकिन पति ने जगह और धन की कमी के कारण अपनी पत्नी को दूर रखने की लगातार इच्छा व्यक्त की है।
विचारण न्यायालय ने पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसके गवाहों द्वारा दिए गए सभी बयानों की पुष्टि नहीं हुई थी, जो उसके करीबी रिश्तेदार होने के कारण अविश्वसनीय भी हैं। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष के गवाह की गवाही को अधिक विश्वसनीय पाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पति को पत्नी/अपीलकर्ता को छोड़ने वाला नहीं कहा जा सकता।
तथ्यों और बयानों की बारीकी से जांच करने पर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मानना था कि अपीलकर्ता के गवाहों द्वारा दिए गए बयान पर्याप्त रूप से पुष्ट थे और वह खुद उनके साथ रहने से पीछे नहीं हटी। यह तथ्य कि पति ने उसे छोड़ दिया था, उसके पिता द्वारा प्रतिवादी को भेजे गए सभी पत्रों से पुष्ट होता है। उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के फैसले को पुष्ट करना कठिन लगा कि और किस तरह के पुष्टीकरण की आवश्यकता हो सकती थी। उच्च न्यायालय अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता के गवाहों द्वारा दी गई गवाही विश्वसनीय है और यह तय करने का कोई कारण नहीं था कि पत्नी खुद ही प्रतिवादी के साथ वैवाहिक संबंध से पीछे हट गई

मुद्दा
इस मामले में जो मुख्य कानूनी मुद्दा उठा, वह यह था कि क्या पत्नी ने खुद ही अपने पति यानी प्रतिवादी के साथ वैवाहिक संबंध से खुद को अलग कर लिया था। न्यायालय ने कानूनी मुद्दे का उत्तर देने का प्रयास किया कि जब यह आरोप लगाया जाता है कि पति या पत्नी ने खुद को वैवाहिक संबंध से अलग कर लिया है, तो सबूत पेश करने का भार किस पर है?
बहस
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने उसे उसके माता-पिता के घर पर छोड़ दिया और उसके माता-पिता के कई पत्रों और अनुरोधों के बावजूद, प्रतिवादी उसे वापस नहीं लेना चाहता था। प्रतिवादी ने जगह की कमी और धन की कमी के कारण उसे अपने साथ रहने का अवसर देने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने कहा कि अपीलकर्ता के साथ क्रूरता का कोई मामला नहीं हुआ है और उसने उसे नहीं छोड़ा है। प्रतिवादी के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपनी मर्जी से उसे छोड़ा था। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने उसे छोड़ दिया और खुद को उसके समाज से अलग कर लिया।
निर्णय
उच्च न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा कि यह तब एक उपाय है जब पति या पत्नी में से कोई एक, बिना किसी उचित आधार के, दूसरे के समाज से खुद को अलग कर लेता है। ऐसी स्थिति में, पीड़ित पति या पत्नी के पास वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर करने का उपाय है और जब अदालत पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और बयानों के आधार पर की गई दलीलों पर विश्वास करती है, तो वह वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक डिक्री दे सकती है, बशर्ते कि ऐसी राहत से इनकार करने का कोई कानूनी आधार न हो।
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका को पुष्ट करने में सक्षम होने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के समाज से स्वेच्छा से खुद को अलग कर लिया है। यहाँ, समाज का अर्थ वैवाहिक समाज है, और इसलिए याचिकाकर्ता पर अपने स्वयं के तर्कों के आधार पर मामले में सफल होने का दायित्व है, न कि प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए बचाव की कमज़ोरी से। अधिनियम 1197 में संशोधन के बाद धारा 9 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण केवल साक्ष्य का एक नियम है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी के लिए याचिकाकर्ता के समाज से अलग होने का कोई उचित आधार था या नहीं, इस प्रश्न के संबंध में सबूत का भार उस पक्ष पर है जो बहाना या आधार प्रस्तुत कर रहा है। इन मामलों में सबूत का भार भारी नहीं है क्योंकि पति-पत्नी से एक-दूसरे के साथ रहने की अपेक्षा की जाती है और जो व्यक्ति अलग रहने का विकल्प चुनता है, उसे ऐसी स्थितियों के अस्तित्व को साबित करना होता है, जिसने उसके लिए यह निर्णय लेने के लिए उचित आधार बनाए। उस समय, यह साबित करने का भार स्वाभाविक रूप से पक्ष पर आ जाएगा कि उसने उचित आधार पर दूसरे की संगति से खुद को अलग कर लिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी के साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि उसके अपने जीवनसाथी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और वह उसे वापस लेने तथा सहवास पुनः आरंभ करने के लिए तैयार है। मुद्दा जो अपने आप में स्पष्ट है वह यह है कि प्रतिवादी उसे भोपाल में रखने के लिए तैयार है या बीना में। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में न तो पति ने पत्नी की पवित्रता पर हमला किया और न ही पत्नी ने पति पर विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया। यदि विचारण न्यायालय ने पत्नी द्वारा मांगी गई राहत प्रदान कर दी होती, तो पति-पत्नी कुछ ही समय में अपने मतभेद पुनः आरंभ कर सकते थे। वैवाहिक संगति का अभाव एक ऐसी समस्या है जो अधिकांश वैवाहिक संबंधों में अत्यंत सामान्य है तथा यह ऐसी चीज है जिसकी चाहत दोनों लिंगों के लोगों को समान रूप से होती है। इससे अक्सर उनके बीच मामूली विवाद पैदा हो जाते हैं। वैवाहिक संबंधों के हित को बनाए रखने के लिए जल्दबाजी में अलगाव और तलाक के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करना महत्वपूर्ण है।
न्यायालय का मानना है कि ऐसा कोई आधार नहीं है कि पत्नी को अपने पति को क्यों त्यागना चाहिए और अपने माता-पिता के संसाधनों पर निर्भर रहना क्यों चुनना चाहिए। अपीलकर्ता ने ईमानदारी दिखाई है और अपने पति के साथ वैवाहिक सहवास को फिर से शुरू करने और ऐसे सहवास में अपेक्षित सभी अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने की सच्ची इच्छा रखती है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ पत्नी शिक्षित और स्वतंत्र दिखती है। पत्नी और कुछ नहीं चाहती, बस अपने पति और उसके दिल के करीब रहना चाहती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करके, यदि वह पूर्णता प्राप्त कर सकती है, तो न्यायालय को उसे वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के माध्यम से पर्याप्त सहारा प्रदान करना चाहिए। इस तर्क के आधार पर उच्च न्यायालय ने माना कि अपील को अनुमति दी गई थी और विचारण न्यायालय के विवादित आदेश को अलग रखा गया था और साथ ही न्यायालय ने अधिनियम की धारा 9 के तहत पत्नी/अपीलकर्ता के पक्ष में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दिया था, साथ ही लागतों का भुगतान अपीलकर्ता को अपील की लागत के रूप में प्रतिवादी द्वारा किया जाना चाहिए।
हरविंदर कौर बनाम हरमंदर सिंह चौधरी (1983)
तथ्य
इस मामले में , वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों के विवरण में जाने के बजाय मुख्य रूप से कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में धारा 9 की संवैधानिकता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियों को सीमित कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो पति ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग की थी और पत्नी ने इसका विरोध किया था। जिला न्यायालय ने पति को वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दिया और उसी आदेश के खिलाफ अपील की गई जिसमें पत्नी ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
मुद्दा
इस मुद्दे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जो यह है कि क्या ऐसे पति या पत्नी को, जिसे दूसरे पति या पत्नी ने त्याग दिया है या छोड़ दिया है, उपचार के रूप में वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना प्रदान करने का प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

निर्णय
उच्च न्यायालय के अनुसार, किसी को यह समझना चाहिए कि न्यायालय किसी साथी को यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है और न ही कभी करेगा। यह तर्क कि वैवाहिक अधिकारों को पुनर्स्थापित करके न्यायालय पति/पत्नी की सहमति के बिना उसे यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य कर रहा है, बेमानी है क्योंकि वैवाहिक अधिकार केवल संभोग से कहीं अधिक हैं। न्यायालय ने स्वीकार किया कि यौन संबंध विवाह और वैवाहिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन यह भी सच है कि वे विवाह का सार नहीं हैं और न ही वैवाहिक जीवन और आनंद के अन्य पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। विवाह को हमेशा संतान प्राप्ति और बच्चों की शिक्षा के लिए एक तंत्र के रूप में देखा गया है, लेकिन इसके साथ ही आपसी समाज, शक्ति और समर्थन, सुख-दुख में साथ देने के उद्देश्य भी हैं। विवाह सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है जिसमें एक व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसका उद्देश्य उन दोनों को लाभ पहुँचाना है और साथ ही तीसरे पक्ष और उनकी आम संतान को भी लाभ पहुँचाना है।
न्यायालय ने एक उदाहरण दिया जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति का घर उसका किला (कैसल) और गढ़ (फॉर्ट्रेस) होता है। पति-पत्नी अपने घर के दरवाजे के भीतर सुरक्षा के लिए छत की मांग कर सकते हैं, जिसे किसी भी नागरिक संस्था और प्राधिकरण को किसी भी तरह से भेदने में सक्षम नहीं होना चाहिए। पति और पत्नी के घरेलू संबंधों की तहों में संवैधानिक कानून का प्रभाव रिश्ते की नींव को प्रभावित करेगा। घरेलू संबंधों पर संवैधानिक सिद्धांतों को इस तरह थोपने से मुकदमेबाजी की बहुलता होगी और वैवाहिक संबंधों की पवित्रता को चुनौती मिलेगी। इससे उन सुरक्षा और सुरक्षा उपायों पर हमला होगा जिन पर वैवाहिक संबंध निर्भर करते हैं। न्यायालय विधायिका की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठा सकते, बल्कि उसे लागू कर सकते हैं और संसद द्वारा इच्छित कानूनों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। यदि विवाह में सुलह विफल हो जाती है, तो भरण-पोषण का सवाल सामने आता है।
इसलिए, न्यायालय का मानना है कि विवाह के पूरी तरह से टूट जाने की स्थिति में भागीदारों के पास पर्याप्त संसाधन हैं और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय ने उन्हें आपसी मतभेदों के बावजूद एक-दूसरे के साथ सहवास फिर से शुरू करने के लिए मजबूर किया। इसलिए, इन सभी कारकों के आधार पर, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि धारा 9 संवैधानिक रूप से शून्य नहीं है। इस मामले में, न्यायालय ने फैसला किया कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एक डिक्री जोड़ों को एक साथ रहने के लिए एक प्रलोभन के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन न्यायालय किसी भी पक्ष को एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वैवाहिक संबंधों का सार इस निर्णय के विवरण में विधिवत संबोधित और कवर किया गया है।
वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की संवैधानिकता को हाल ही में दी गई चुनौती
हाल ही में, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के छात्रों ने 2019 में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें विभिन्न पारिवारिक कानूनों के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की संवैधानिकता को चुनौती दी गई, लेकिन मुख्य रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 को चुनौती दी गई थी। इस मामले को ओजस्व पाठक बनाम भारत संघ (2019) के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह अनिर्णीत (अंडिसाइड) है। चुनौती के आधार काफी हद तक एक महिला की शारीरिक स्वायत्तता (ऑटोनोमी) के आधार पर थे। याचिका में कहा गया है कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश एक महिला की स्वायत्तता के खिलाफ है; यह उसे अपने पति के घर लौटने के लिए मजबूर करता है जहाँ उसे किसी तरह की क्रूरता या दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। विवाद का दूसरा प्राथमिक आधार एक महिला की यौन स्वायत्तता के बारे में है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश एक महिला की यौन स्वायत्तता को प्रभावित करता है और उसे ऐसी स्थिति में मजबूर करता है, जहां उसे अपनी मर्जी के बिना अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि सम्पादन (कंज्यूमेशन) और संभोग सहवास के अभिन्न अंग हैं। उनका कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है क्योंकि यह महिला के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है, चुनौती का अंतिम आधार यह है कि कानून का अनुप्रयोग काफी हद तक असमान है और महिलाओं पर भारी और असमान बोझ डालता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है जो समानता के अधिकार और भेदभाव के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। मामला अभी भी अदालतों के समक्ष लंबित है और फैसला आना बाकी है, लेकिन यह वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की वैधता पर चर्चा को आकार देगा।

निष्कर्ष
वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना और इसकी वैधता के बारे में दो विचारधाराएँ हैं, लेकिन भारतीय कानूनी व्यवस्था में यह अभी भी संवैधानिक है। रूढ़िवादी विचारधारा का मानना है कि वैवाहिक संबंधों और संस्थाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पति या पत्नी के परित्याग या त्याग के खिलाफ यह एक आवश्यक राहत है, जबकि नारीवादी विचारधारा का मानना है कि यह एक महिला की निजता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। वैवाहिक राहत की वैधता पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के अलग-अलग विचार रहे हैं, लेकिन अंततः सरोज रानी बनाम सुदर्शन चड्ढा (1984) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा और महसूस किया कि वैवाहिक संबंधों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है। आगे यह देखना बाकी है कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के प्रावधानों को हाल ही में दी गई चुनौती पर निर्णय लेते समय सर्वोच्च न्यायालय की राय बदलेगी या नहीं। परिणाम जो भी हो, वैवाहिक संबंधों और राहतों से निपटने के दौरान एक समतावादी समाज और विवाह की समकालीन संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है। बहरहाल, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निश्चित रूप से अब तक के कई अन्य न्यायिक निर्णयों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू)
वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या साबित करना होगा?
याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण या आधार के अपने आप को उसके समाज से अलग कर लिया तथा तब से उसके साथ सहवास पुनः शुरू नहीं किया।
वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से इनकार करने के उचित आधार क्या हैं?
वैवाहिक राहत से संबंधित आधारों पर वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से इनकार किया जा सकता है, जैसे क्रूरता, शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार, कदाचार, पति की नपुंसकता, मानसिक पागलपन, घरेलू हिंसा, पुनर्विवाह या द्विविवाह।
क्या होता है जब पुनर्स्थापना का आदेश पारित कर दिया जाता है लेकिन प्रतिवादी उसका अनुपालन नहीं करता?
जब प्रतिवादी या निर्णय ऋणी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो न्यायालय उनकी संपत्ति कुर्क कर सकता है और यदि ऐसी कुर्की के छह महीने के भीतर अनुपालन नहीं दिखाया जाता है, तो उसे बेच सकता है।
क्या होता है जब पुनर्स्थापना का आदेश पारित कर दिया जाता है लेकिन आदेश धारक उसका अनुपालन नहीं करता?
जब डिक्री धारक स्वयं पुनर्स्थापन के लिए डिक्री का अनुपालन नहीं करता है, तो वह तलाक जैसी किसी अन्य राहत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून के सिद्धांतों और प्रावधानों के अनुसार उसे अपने द्वारा किए गए गलत कार्य का लाभ उठाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
कौन सा न्यायालय वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के मामलों पर विचार करता है?
आमतौर पर, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा पारिवारिक न्यायालयों द्वारा किया जाता है।
संदर्भ







