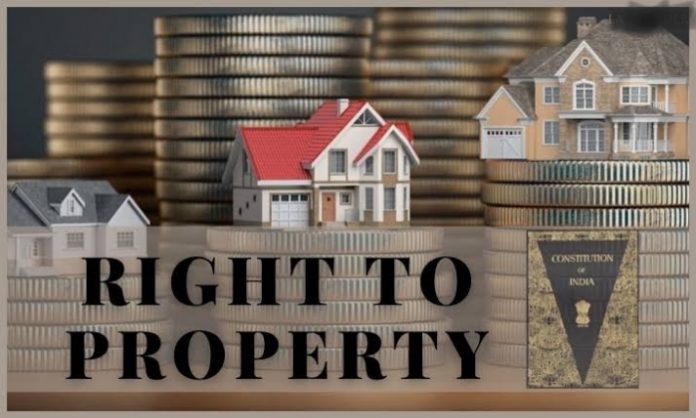यह लेख Shweta Singh द्वारा लिखा गया है। इस लेख में मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी शामिल है। इसमें संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार से लेकर संवैधानिक अधिकार के रूप में अपमानित होने तक के विकास पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा, यह संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत इस अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के पीछे के कारणों और किस कारण से सरकार ने इसे हटा दिया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में पुनः वर्गीकृत किया, को भी बताता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के आगमन के बाद से संपत्ति के अधिकार को हमेशा एक मौलिक अधिकार माना गया है। हालाँकि, इस अवधारणा का अर्थ और महत्व पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है। यह लेख भारत के संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के विकास और प्रभावों की पड़ताल करता है। इससे पहले, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया था। हालाँकि, 1978 में, संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम ने इसे कानूनी अधिकार के रूप में बदल दिया और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण भूमि सुधारों में बदलाव के कारण इसे अनुच्छेद 300A के तहत रखा गया। इसने सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में कानून पारित करने में सक्षम बनाया है, जिससे भूमि मालिकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, इसने सार्वजनिक कल्याण के साथ निजी संपत्ति अधिकारों के संतुलन पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरे, विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों और मामले, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रावधानों ने, संपत्ति के अधिकार के दायरे और प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) को बढ़ाया है।
संपत्ति के अधिकार का इतिहास
संपत्ति के अधिकार विकसित हुए हैं और उन्होंने मानव सभ्यताओं की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक समाजों में, संपत्ति के अधिकार अक्सर कब्जे और उपयोग पर आधारित होते थे। खानाबदोश (नोमेडिक) जनजातियों ने व्यक्तिगत संपत्ति जैसे कपड़े, उपकरण और यहां तक कि हथियार भी स्वीकार किए। हालाँकि, निजी संपत्ति की अवधारणा प्रतिबंधित थी, उनमें से अधिकांश ने सामुदायिक स्वामित्व की अवधारणा का पालन किया। मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसे अधिक उन्नत समाजों के विकास के साथ, संपत्ति अधिकारों की अधिक जटिल प्रणालियाँ विकसित हुईं। भूमि का स्वामित्व मुख्य रूप से शासक वर्ग या राज्य के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि व्यक्तियों को कृषि या किसी अन्य उद्देश्य जिसे वे उचित समझते थे के लिए भूमि का उपयोग करने का विशेषाधिकार था। संपत्ति के अधिकार सामाजिक स्तर से दृढ़ता से जुड़े हुए थे और सत्ता में बैठे लोग इन्हें छीन सकते थे। मध्य युग के दौरान यूरोप में सामंतवाद (एग्लेटेरियन) का उदय हुआ। राजा सैन्य सेवा और वफादारी के बदले में अमीरों को जमीन देते थे। संपत्ति के अधिकार भूमि वितरण और नियंत्रण को नियंत्रित करने वाले सख्त पदानुक्रमों के साथ, मालिक और नौकरों के बीच संबंधों के आसपास संरचित किए गए थे।
जहां तक भारत में संपत्ति के अधिकारों का संबंध है, वे किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष जाति में प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं द्वारा शासित होते हैं। संपत्ति कुलों या समुदायों के सदस्यों के माध्यम से विरासत में मिली थी, और व्यक्तिगत संपत्ति का स्वामित्व आम नहीं था। संपत्ति का विचार सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। मध्यकाल में कुलीनों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि देने की प्रथा थी। राज्य या शासक अभिजात वर्ग के पास बड़ी मात्रा में भूमि का स्वामित्व था, और किसानों से कर वसूलने के लिए भूमि राजस्व प्रणाली बनाई गई थी। ब्रिटिश शासन का भारत में संपत्ति के अधिकारों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। बंगाल में 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने ब्रिटिश कानून के तहत निजी संपत्ति के स्वामित्व की अवधारणा की शुरूआत को प्रभावित किया, जहां जमींदारों को ब्रिटिश ताज के लिए निश्चित राजस्व के बदले में भूमि पर स्थायी अधिकार दिए गए थे। रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था (ये व्यवस्था भूमि पर करों के माध्यम से उत्पन्न राजस्व को नियमित करने का एक तरीका था) को बाद में भारत के अन्य हिस्सों में विस्तारित किया गया। व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व स्थापित किया गया, किसानों को ब्रिटिश प्रशासन या अन्य मध्यस्थों (इंटरमीडियरी) को भूमि और राजस्व का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा, स्वतंत्रता के बाद, संपत्ति के अधिकारों को मानव विकास के एक अनिवार्य पहलू के रूप में मान्यता दी गई और इसलिए संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के भाग III के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया।

संपत्ति के अधिकार का विकास
भारत का संविधान अपने प्रावधानों को 1935 के भारत सरकार अधिनियम और 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा से प्राप्त करता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अधिनियम की धारा 299 के तहत संपत्ति के अधिकार के प्रावधान शामिल थे, जिसमें सार्वजनिक हित के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अनिवार्य अधिग्रहण से संपत्ति की सुरक्षा शामिल थी। उसी तरह, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि हर किसी को संपत्ति रखने का अधिकार है।
भारत का संविधान बनाते समय, संविधान सभा ने कई देशों के संविधानों के प्रावधानों पर ध्यान दिया, जो नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग करते थे। यह कहा गया है कि संविधान आम तौर पर कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म, सभा, संघ, व्यक्तिगत सुरक्षा और संपत्ति से संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है। सीमा के भीतर, इन अधिकारों को मौलिक और अच्छी तरह से स्थापित माना गया। अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के मसौदे पर संविधान सभा सत्र के दौरान हुई बहस ने साबित कर दिया कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संपत्ति के अधिकार को काफी महत्व दिया था। उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में रखा, जिससे नव निर्मित राज्य में संपत्ति के अधिकारों पर निष्पक्ष और उचित विचार की गारंटी देने की उनकी उत्सुकता दिखाई दी। मूल रूप से, 1978 तक, संपत्ति का अधिकार भारत में मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा था। हालाँकि, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बन गया।
मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार
संविधान सभा ने एक ऐसी कानूनी प्रणाली की कल्पना की जो लोकतांत्रिक समाजवाद और उदार (लिबरल) लोकतंत्र का एक अनूठा मिश्रण थी। इस प्रणाली से अपेक्षा की गई थी कि यह भूमि सुधार और संसाधन वितरण सहित सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में काम करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगी। हालाँकि, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने के उद्देश्य से भूमि पुनर्वितरण पर नीति शुरू करने के बीच विवाद था। इससे संविधान सभा के भीतर बहस शुरू हुई और अंततः, इन दो प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित हुआ। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान के भाग III के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को अपनाया गया।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f)
जैसा कि प्रारंभ में अपनाया गया था, अनुच्छेद 19(1)(f) भारत के सभी नागरिकों को “संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने” के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि, इस अधिकार को जनता के हित में संघ और राज्य विधानसभाओं द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) में दिया गया है।
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल बोस (1953) के मामले में मुख्य न्यायाधीश शास्त्री ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) से संबंधित एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 19(1)(f) व्यापक अर्थों में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के नागरिक के सामान्य अधिकार पर केंद्रित था, न कि संपत्ति के स्वामित्व के विशिष्ट उदाहरणों पर। उनकी व्याख्या के अनुसार, अनुच्छेद 19(1)(f) ने संपत्ति के अमूर्त अधिकार की रक्षा की, जिसका अर्थ है कि यह मौलिक सिद्धांत की गारंटी देता है कि नागरिकों को संपत्ति से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होने की स्वतंत्रता है। इस लेख में संपत्ति के किसी विशेष टुकड़े से जुड़े अधिकारों के संबंध में कुछ भी पता नहीं लगाया गया है। इस परिवर्तन में निहित है कि यह स्थापित किया गया था कि नागरिकों के पास संपत्ति का सामान्य अधिकार था, विशेष संपत्ति अधिकारों को अभी भी अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना कानून और विनियमों द्वारा विनियमित किया जा सकता है।
आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती (एंडोमेंट) बनाम लक्ष्मींद्र (1954) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत शामिल ‘संपत्ति’ शब्द का उदार निर्माण किया। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई तर्क नहीं है जो ‘संपत्ति’ की एक संकीर्ण परिभाषा में केवल भौतिक या मूर्त संपत्तियों को शामिल करने की गारंटी दे। साथ ही, इस शब्द में विभिन्न प्रकार के हित भी शामिल होने चाहिए जो मालिकाना अधिकारों की कुछ विशेषताओं से मिलते जुलते हों। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 19(1)(f) न केवल विशिष्ट भौतिक संपत्तियों पर बल्कि अधिक अमूर्त संपत्ति अधिकारों पर भी लागू होता है।
इसी तरह, अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31(2) के तहत ‘संपत्ति’ के दायरे और परिभाषा को सर्वोच्च न्यायालय ने एम. एम. पाठक बनाम भारत संघ (1978) के मामले में आगे समझाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘संपत्ति’ हर प्रकार की संपत्ति को संदर्भित करती है, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त। इसमें न केवल मूर्त वस्तुएँ और भूमि, बल्कि ऋण और अन्य वित्तीय हित भी शामिल थे, या जिसे “कार्यों में विकल्प” कहा जाता था। इसलिए, इन संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत सुरक्षा को संपत्ति के प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला तक बढ़ाया गया था, जिससे संपत्ति के अधिकारों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया था जिसमें भौतिक संपत्ति और अमूर्त हित दोनों शामिल थे।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 299 पर आधारित था। हालाँकि, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में किसी व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों को प्रदान की गई सुरक्षा के समग्र संतुलन को प्रभावित किया है। 1935 अधिनियम की धारा 299 ने अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति पर कुछ प्रतिबंधों को संवैधानिक दर्जा दिया था। इस तरह के प्रतिबंध औपनिवेशिक (कोलोनियल) कानून के एक सेट से उत्पन्न हुए, जो 1824 के बंगाल विनियमन अधिनियम I से शुरू हुआ और 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के साथ समाप्त हुआ। इन औपनिवेशिक कानूनों ने निजी संपत्ति पर राज्यों के नियंत्रण पर कुछ प्रतिबंध लगाने की मांग की, और इसलिए ऐसी संपत्ति के मालिकों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई। संपत्ति अधिकारों की कुछ श्रेणियों को बेहतर सुरक्षा मिली, जिससे यह गारंटी मिली कि विशिष्ट प्रकार की संपत्ति को राज्य द्वारा आसानी से जब्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, अन्य प्रकार के संपत्ति अधिकारों को कम सुरक्षित बना दिया गया ताकि राज्य उन स्थितियों में आसानी से भूमि पर कब्जा कर सके जहां ऐसी कार्रवाई सार्वजनिक हित में आवश्यक समझी जाती है।
अनुच्छेद 31 का मसौदा तैयार करने पर संविधान सभा की बहस निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित थी:
- व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार और सामाजिक और आर्थिक सुधारों की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
- क्या ‘सार्वजनिक उद्देश्य’ शब्द को आधिकारिक सरकारी उद्देश्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, या महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों को शामिल करने के लिए इसकी व्यापक और अधिक लचीले अर्थ में व्याख्या की जानी चाहिए?
- संपत्ति का ‘अधिग्रहण’ या ‘वंचन’ (डेप्रिवेशन) किसे माना जा सकता है जिसके लिए मुआवजे की आवश्यकता होगी?
- ‘मुआवजा’ का क्या मतलब है और कोई ‘उचित’, और ‘न्यायसंगत’ जैसे शब्दों को कैसे परिभाषित करता है?
- मुआवज़े की राशि के साथ-साथ इसका वितरण कैसे किया जाएगा, इस पर अंतिम निर्णय लेने वाला कौन होगा?
अंततः संविधान सभा द्वारा अपनाए गए अनुच्छेद 31 के प्रावधान में यह प्रावधान किया गया कि “कानून के अधिकार के अलावा किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।” इसके अलावा, अनुच्छेद 31(2) में प्रावधान है कि चल (जैसे वाहन या मशीनरी) और अचल संपत्ति (जैसे भूमि या भवन) दोनों, जिसमें ऐसी संपत्ति में या वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रमों (अंडरटेकिंग) के स्वामित्व वाली कंपनियों में कोई हित शामिल है, केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही अधिग्रहण किया जा सकता है और ऐसे अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानून में मुआवजे का भी प्रावधान होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसा कानून या तो मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि को निर्दिष्ट कर सकता है या ऐसे सिद्धांत या तरीके प्रदान कर सकता है जिनका उपयोग मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। अनुच्छेद 31(3) में आगे प्रावधान है कि अनुच्छेद 31(2) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून तभी प्रभावी होगा जब इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया हो और उनकी सहमति प्राप्त हुई हो। ऐसे प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कानूनों को लागू होने से पहले उच्चतम स्तर पर जांच की जाए। अनुच्छेद 31(4) के तहत कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें प्रावधान है कि यदि संविधान लागू होने के समय कुछ कानून विधायी प्रक्रिया में थे, तो ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होंगे। इसमें आगे प्रावधान है कि यदि कोई विधेयक, जो संविधान लागू होने के समय लंबित था, उसके बाद विधायिका द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, तो ऐसे कानून को अदालत के समक्ष इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह अनुच्छेद 31(2) के तहत प्रदान की गई मुआवजे की आवश्यकता के अनुपालन में नहीं है। हालाँकि, अनुच्छेद 31(2) के दो अपवाद हैं और उन्हें अनुच्छेद 31(5) के तहत प्रदान किया गया है। वे इस प्रकार हैं:
- मौजूदा कानून, अनुच्छेद 31(6) के तहत निर्दिष्ट कानूनों को छोड़कर, अनुच्छेद 31(2) से प्रभावित नहीं होते हैं।
- कर या जुर्माना लगाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य का समर्थन करने और जीवन या संपत्ति के खतरे को रोकने के उद्देश्य से राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 31(2) के दायरे से बाहर रखा गया है। कुछ समझौतों के तहत निष्क्रांत संपत्ति से संबंधित अन्य कानून भी अनुच्छेद 31(2) के अपवाद के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद 31(6) द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी राज्य कानून जो इस संविधान के प्रारंभ होने के 18 महीने के भीतर अधिनियमित किया गया था, उसे इस संविधान के शुरू होने के 3 महीने के भीतर प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि जहां राष्ट्रपति ने ऐसे कानून को प्रमाणित किया है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर असंवैधानिक के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह अनुच्छेद 31(2) या भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 299(2) का उल्लंघन करता है।
अनुच्छेद 31 के खंड (1) और (2) की भावना भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 299(1) और (2) के समान थी, लेकिन दो मामलों में थोड़ा अंतर था। सबसे पहले, धारा 299 संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण की सीमा तक ही सीमित थी, जबकि अनुच्छेद 31 ने इसे ‘सार्वजनिक उपयोग’ के लिए संपत्ति पर कब्ज़ा करने के मामलों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया। इसका तात्पर्य यह था कि मुआवजे का भुगतान इस बात की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए कि संपत्ति का स्वामित्व सरकार में निहित है या नहीं। दूसरा, जबकि संविधान के अनुच्छेद 31(2) में प्रावधान है कि विधायिका बॉन्ड सहित किसी भी अन्य रूप में मुआवजे की अनुमति दे सकती है, धारा 299(2) में प्रावधान है कि मुआवजा केवल धन के रूप में होना चाहिए। अनुच्छेद 31(4) और 31(6) विशेष रूप से भूमि सुधार कानूनों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए बनाए गए थे। उन्होंने कुछ शर्तें रखीं जिनके तहत अनुच्छेद 31 के खंड (1) और (2) में निर्धारित संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया कि किन संपत्ति अधिकारों या हितों को बाहर रखा गया है। इसके बजाय, उन्होंने कुछ निश्चित अवधियों की ओर इशारा किया जब कानून पारित किया गया था जो अनुच्छेद 31(2) की आवश्यकताओं से मुक्त होगा। जबकि खंड (4) उन विधेयकों से कानून को छूट देता है जो संविधान लागू होने के समय संसद के समक्ष थे, खंड (6) ने संविधान के शुरू होने के 18 महीने के भीतर पारित कानून को बाहर रखा। दोनों प्रकार के कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाना था, इस प्रकार संघ कार्यकारी की सहमति निहित थी।
संवैधानिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार
भूमि सुधार और राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाते हुए संपत्ति के मौलिक अधिकार की गारंटी ने एक पूर्वानुमानित विवाद पैदा कर दिया। जबकि विधायिका और कार्यपालिका ने विकास परियोजनाओं को लागू करने की मांग की, न्यायपालिका ने इन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा की। वर्षों से इस स्थिति के कारण न्यायपालिका ने भूमि सुधार जैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए बने कई कानूनों को रद्द कर दिया। इस न्यायिक प्रतिवाद ने विधायिका से कई संवैधानिक संशोधन करने का आग्रह किया। 1978 के 44वें संशोधन ने संविधान के ‘मौलिक अधिकारों’ से संबंधित अनुभाग से अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटा दिया और एक नए अध्याय में अनुच्छेद 300A को शामिल किया। इस परिवर्तन ने ‘संपत्ति के अधिकार’ को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया।
भारतीय संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार में संशोधन
भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों में संविधान की स्थापना के बाद से कुल छह बार संशोधन किया गया है।
पहला संशोधन अधिनियम (1951)
प्रारंभिक वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा भूमि सुधारों का उद्देश्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची II, प्रविष्टि 18) के अनुसार, भूमि एक ऐसा विषय है जो किसी राज्य की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि केवल राज्य विधानसभाएं ही इसके संबंध में कानून बना सकती हैं। 1950 के बिहार भूमि सुधार अधिनियम और 1950 के उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को असंवैधानिक होने के कारण अदालत में चुनौती दी गई। प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दिए गए मुख्य तर्क यह थे कि ये अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में दिए गए संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि अधिग्रहण किसी सार्वजनिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं थे, और प्रस्तावित मुआवजा कम और अवास्तविक था। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य (1951) के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 1950 का बिहार भूमि सुधार अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत प्रदान किए गए संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है, जबकि दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजा सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1951) के मामले में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 की वैधता को बरकरार रखा। इन परस्पर विरोधी निर्णयों को अंतिम निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजा गया। जब ये अपीलें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थीं, अनंतिम संसद ने 1951 का संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम पारित किया।
संपत्ति के अधिकार का ऐतिहासिक विकास प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 के साथ शुरू हुआ, जिसमें अनुच्छेद 31-A और 31-B को संविधान में शामिल किया गया और यहां तक कि नौवीं अनुसूची भी पेश की गई। संशोधनों का उद्देश्य कुछ ऐसा करना था जो मूल अनुच्छेद 31 में शामिल नहीं था। उन्होंने संपत्ति हितों के उन प्रकारों की गणना की जिन्हें अनुच्छेद 31(2) और अनुच्छेद 14 और 19 के तहत शामिल अन्य प्रावधानों के तहत मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता से छूट नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 31A(1) का आशय यह था कि किसी संपत्ति में किसी अधिकार के अधिग्रहण के लिए या ऐसे अधिकारों में परिवर्तन या निरसन के लिए कानून बनाने की राज्य की क्षमता को भारत के संविधान के भाग III के तहत निहित किसी भी प्रावधान के साथ असंगत होने के कारण रद्द नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 31A(2) में ‘संपत्ति’ शब्द का अर्थ समझाया गया है। अनुच्छेद 31A2(a) को यह कहते हुए चित्रित किया गया है कि “संपत्ति” का वही अर्थ है जो भूमि के कार्यकाल के संबंध में स्थानीय कानूनों में है और इसमें “जागीर, इनाम, मुआफी या कोई समान अनुदान” शामिल है। अनुच्छेद 31A2(b) ने स्पष्ट किया कि संपत्ति से संबंधित अधिकारों में मालिकों, उप-मालिकों, कार्यकाल धारकों, मध्यस्थों और किसी भी अन्य अधिकार और विशेषाधिकारों के अधिकार शामिल हैं जहां तक भूमि राजस्व का संबंध है।
प्रथम संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 31-B और नौवीं अनुसूची भी पेश की। अनुच्छेद 31B में प्रावधान है कि नौवीं अनुसूची में शामिल कोई भी कानून केवल इसलिए रद्द नहीं किया जाएगा या शून्य नहीं माना जाएगा क्योंकि इसे संविधान के भाग III के तहत संरक्षित किसी भी अधिकार के साथ टकराव में घोषित किया गया था। इसका मतलब यह था कि अनुच्छेद 13(1), जिसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों के विपरीत कोई भी कानून असंगतता की सीमा तक शून्य होगा, नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानूनों पर लागू नहीं होता है।
नए कानूनों को संशोधनों के माध्यम से नौवीं अनुसूची में शामिल करने की प्रथा के परिणामस्वरूप संरक्षित कानूनों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रारंभ में, 64 कानून थे जिन्हें नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बाद के संशोधनों ने इस प्रवृत्ति को जारी रखा: चौथे संशोधन द्वारा 17 नए कानून जोड़े गए; 17वें संशोधन में 29 नए कानून जोड़े गए; 34वें संशोधन में 17 नए कानून जोड़े गए; 39वें संशोधन में 38 नए कानून जोड़े गए; 42वें संशोधन में 64 नए कानून जोड़े गए; और इसे कुल 202 बनाते हुए 47वें संशोधन द्वारा 14 नए कानून जोड़े गए। केवल 1993 में, 66वें संशोधन के माध्यम से, 55 विधानों को जोड़ा गया जिससे कुल विधानों की संख्या 257 हो गई। 1994 के 75वें संशोधन अधिनियम में एक तमिलनाडु अधिनियम भी शामिल था जिसमें नौवीं अनुसूची के तहत पिछड़े वर्गों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण की परिकल्पना की गई थी। नौवीं अनुसूची के इस विस्तारित उपयोग की इसके मूल उद्देश्य से विचलन के रूप में आलोचना की गई है, जो भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक चुनौतियों से बचाना था। 1995 में 78वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 27 और अधिनियम शामिल किये गये, जिससे कुल 284 अधिनियम हो गये।
श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य और अन्य (1951) (इसके बाद ‘संकरी प्रसाद मामला’ के रूप में संदर्भित), में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का विशेष अधिकार था।

इसके अलावा, न्यायालय ने बताया कि यह प्रावधान कि कानून अनुच्छेद 13(2) के तहत उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कम नहीं करेगा या छीन नहीं लेगा, संविधान में संशोधन करने वाले कानूनों पर लागू नहीं है। इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने वाला संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत असंवैधानिक नहीं माना गया था।
चौथा संशोधन अधिनियम (1955)
नौवीं अनुसूची की शुरुआत के बाद, विधायिका ने अपनी शक्ति के प्रयोग पर न्यायपालिका की जांच को दरकिनार करने के लिए नौवीं अनुसूची में कई कानून जोड़े। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार के मुद्दे पर वादियों के पक्ष में कई मामलों का फैसला किया है। इनमें से अधिकांश सफल संवैधानिक चुनौतियों को उन संशोधनों द्वारा हटा दिया गया, जिन्होंने या तो विवादास्पद कानूनों को नौवीं अनुसूची में जोड़ा या संवैधानिक प्रावधानों में और बदलाव किए। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम श्रीमती बेला बनर्जी (1954) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सरकार को भारत के संविधान में चौथा संशोधन पेश करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रमुख मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के हर मामले में मुआवजा देना होगा। न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 31 के खंड (1) और खंड (2) दोनों एक ही मुद्दे को संबोधित करते हैं, यानी निजी संपत्ति से वंचित करना। इसके अलावा, अदालत ने मुआवज़े शब्द की व्याख्या पर ज़ोर देते हुए कहा कि इसका मतलब उचित मुआवज़ा है, जो कि मालिक ने जो खोया है उसके बराबर है।
1955 में, अनुच्छेद 31 के खंड (2) में संशोधन करके और अनुच्छेद 31 में खंड (2-A) को सम्मिलित करके इस निर्णय का मुकाबला करने के लिए संसद द्वारा चौथा संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस परिवर्तन का मतलब यह था कि खंड (2) खंड (2-A) में परिभाषित संपत्ति के अधिग्रहण या मांग को शामिल करता है और खंड (1) अधिग्रहण या मांग के अलावा अन्य तरीकों से राज्य द्वारा संपत्ति के अभाव को रेखांकित करता है। इस संशोधन ने राज्य को कानून द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया। इसने राज्य को अर्जित/मांगी गई संपत्ति के लिए मुआवजे का निर्धारण करने का अधिकार दिया, या तो राशि बताकर या यह बताकर कि इसकी गणना कैसे की जाएगी। संशोधित खंड (2) में आगे प्रावधान किया गया है कि राशि की पर्याप्तता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है, जिससे राज्य को मुआवजे के मामलों पर पर्याप्त विवेक मिलता है।
सत्रहवाँ संशोधन अधिनियम
केरल और मद्रास राज्यों द्वारा किए गए कुछ भूमि सुधारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 31-A और नौवीं अनुसूची के दायरे में संशोधन और विस्तार करने के लिए 1964 का सत्रहवाँ संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 31-A में “संपत्ति” शब्द के अर्थ को बढ़ाकर केरल और मद्रास के साथ-साथ रयोतवारी भूमि में ‘जागीर’, ‘इनाम’, ‘मुआफ़ी’ और ‘जन्मम’ अधिकारों जैसे भूमि कार्यकाल के अन्य रूपों को भी शामिल कर दिया।
इसके अलावा, इसने अनुच्छेद 31-A के खंड (1) में एक और परंतुक जोड़कर संशोधन किया। इस प्रावधान का उद्देश्य लोगों को व्यक्तिगत खेती के लिए रखी गई भूमि सीमा से नीचे की भूमि से बेदखल होने से रोकना था, और यदि ऐसी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, तो यह उसके बाजार मूल्य पर होगी। संशोधन ने नौवीं अनुसूची में 44 और कानून भी जोड़े गए जिससे ये कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानूनी चुनौतियों से प्रतिरक्षित हो गए।
सत्रहवें संशोधन अधिनियम, 1964 द्वारा नौवीं अनुसूची में जोड़े गए कुछ कानूनों की वैधता को अदालत में चुनौती दी गई थी। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) के मामले में इन कानूनों को बरकरार रखा। अपने फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद के पहले मामले में स्थापित मिसाल का पालन किया। न्यायालय ने ‘स्टेयर डेसिसिस’ के सिद्धांत को लागू किया, जिसका अर्थ है पहले से स्थापित फैसलों का पालन करना। इसने कानूनी व्याख्याओं में निरंतरता सुनिश्चित की और सत्रहवें संशोधन अधिनियम के तहत किए गए संशोधनों को बरकरार रखा।
पच्चीसवाँ संशोधन अधिनियम
परिणामस्वरूप, भारतीय संविधान के पच्चीसवें संशोधन में तीन प्रमुख परिवर्तन शामिल थे। सबसे पहले, इसने “मुआवजा” शब्द को “राशि” से बदलने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(2) को संशोधित किया। यह नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को राज्य के स्वामित्व के अधिकार में स्थानांतरित करने का एक प्रयास था। परिणामस्वरूप, राज्य “मुआवजे” के बजाय एक अनिर्दिष्ट “राशि” जो उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए का भुगतान करके किसी की संपत्ति ले सकता है।
दूसरा, संशोधन ने किसी व्यक्ति की संपत्ति को अपने विवेक से और ऐसे नियमों और शर्तों के तहत लेने के लिए राज्य के अधिकार का विस्तार करने की मांग की, जो वह पसंद करेगा। इसका मतलब यह था कि राज्य हमेशा यह तय कर सकता है कि पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने की आवश्यकता के बिना, किसी भी समय और किसी भी शर्त पर संपत्ति के लिए कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए।
तीसरा, संशोधन ने अदालतों को राज्य के आचरण की समीक्षा करने से रोकने का प्रयास किया, भले ही कार्रवाई मनमानी या तर्कहीन हो। इसने राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा को काफी कम कर दिया। पर्याप्त मुआवज़े के बिना संपत्ति का नुकसान अन्य स्वतंत्रताओं को प्रभावित कर सकता है क्योंकि उन्हें सीमित किया जा सकता है, अप्रभावी बनाया जा सकता है, या यहां तक कि उन्हें अस्वीकार भी किया जा सकता है। इस नियम का एकमात्र अपवाद शिक्षा संस्थानों के मामले में था, जैसा कि अनुच्छेद 31(2) के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है।
पच्चीसवें संशोधन में तथाकथित अनुच्छेद 31C भी जोड़ा गया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के तहत उल्लिखित राज्य की नीतियों को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर संवैधानिक रूप से अमान्य करने से रोकता है कि यह अनुच्छेद 14, 19, और 31 के तहत प्रदान किए गए संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, यदि किसी कानून में यह कथन है कि इसका उद्देश्य इन नीतियों को साकार करना है, तो इसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि यह कानून इन नीतियों को साकार नहीं करता है।
भारतीय संविधान का 44वाँ संशोधन अधिनियम
1978 के संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम ने भारत में संपत्ति के अधिकार में बड़े बदलाव पेश किए। इसने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत पहले प्रदान किए गए संपत्ति के अधिकारों को प्रतिस्थापित कर दिया और भारतीय संविधान के भाग XII के एक नए अध्याय IV में अनुच्छेद 300A पेश किया। इस बदलाव का मतलब यह हुआ कि संपत्ति अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि अनुच्छेद 300-A के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि “कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।” इस प्रकार, चवालीसवें संशोधन के अनुसार, राज्य अन्य अनुच्छेद द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, संपत्ति मालिकों को उसके द्वारा ली गई संपत्ति के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 30(1A) कहता है कि जहां अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित संस्था की संपत्ति अर्जित की जाती है, वहां मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी तरह, अनुच्छेद 31A(1) का दूसरा प्रावधान यह बताता है कि, संपत्तियां जहां व्यक्तिगत खेती की जा रही है, उसका अधिग्रहण किया जाता है, तो मुआवजा बाजार मूल्य पर दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप एक अनियमित स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके तहत अनुच्छेद 30(1A) और 31A(1) के कानूनी प्रावधानों के तहत प्रदान की गई विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, ज्यादातर मामलों में राज्य, जब भी सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो मुआवजे के रूप में बाजार मूल्य का भुगतान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं होता है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किये गये:
- अनुच्छेद 19(1)(f) को निरस्त कर दिया गया, जो प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने का अधिकार देता था।
- अनुच्छेद 30 को नए खंड (1-A) के साथ संशोधित किया गया, इस आशय से कि यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक-प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो मुआवजा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करेगा।
- उपशीर्षक “संपत्ति का अधिकार” हटा दिया गया।
- अनुच्छेद 31 हटा दिया गया।
- “संपत्ति का अधिकार” नामक अध्याय IV को शामिल करके भाग XII में संशोधन किया गया, जिसमें अनुच्छेद 300A शामिल है, जिसमें कहा गया है, “किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा”।
- नौवीं अनुसूची को संशोधित किया गया, और विशेष प्रविष्टियाँ 87, 92, और 130 को सूची से हटा दिया गया।

44वें संशोधन अधिनियम के पीछे का कारण
अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटाने और अनुच्छेद 300-A को लागू करने का उद्देश्य संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाना था। इसका मतलब यह है कि हालाँकि संपत्ति का अधिकार अभी भी कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रहेगा, लेकिन विधायिका के हस्तक्षेप से यह सुरक्षित नहीं रहेगा। 1978 में पारित 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को “मौलिक अधिकार” सूची से हटा दिए जाने का एक और कारण यह था कि इस अधिकार ने समाजवाद के एकीकरण और संसाधनों के समान वितरण में कई समस्याएं पैदा कीं।
स्वतंत्रता के बाद, संपत्ति के अधिकार ने भारत में कई कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियाँ पेश कीं। सभी मौलिक अधिकारों में से, संपत्ति का अधिकार सबसे विवादास्पद रहा है और इसने सरकार और नागरिकों के बीच कई कानूनी मुकदमों को जन्म दिया है। जवाब में, केंद्र और राज्य सरकारों ने सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए संपत्ति के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए। कृषि क्षेत्र में, सरकार ने जोतने वालों को संपत्ति का अधिकार देने, जमींदारी प्रथा को हटाने, किरायेदारों को कार्यकाल की सुरक्षा देने, कृषि भूमि की व्यक्तिगत जोत पर एक सीमा लगाने और अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरित करने का प्रस्ताव रखा। शहरी क्षेत्रों में, उन्होंने अपनी गतिविधियों को आवास निर्माण, अवैध आवासीय क्षेत्रों के उन्मूलन, और योजना, किराए के विनियमन, संपत्ति की खरीद और यहां तक कि शहरी भूमि की हिस्सेदारी को सीमित करने पर केंद्रित किया। इसके अलावा, इसका उद्देश्य राष्ट्रीयकरण के माध्यम से व्यावसायिक उद्यमों (वेंचर्स) और वाणिज्यिक (कमर्शियल) गतिविधियों के कुछ पहलुओं को विनियमित करना था। ये सभी विधायी कार्य समाज में समाजवादी संरचना स्थापित करने की दृष्टि से किये गये थे। इसलिए, इन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए भारत के संविधान के भाग III से अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) को हटा दिया गया था।
44वें संशोधन अधिनियम के परिणाम
भारतीय संविधान को अपनाने के समय, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा था। हालाँकि, 1978 में, 44वें संशोधन अधिनियम ने इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और अनुच्छेद 300-A की शुरूआत के साथ इसे संवैधानिक अधिकार करार दिया। इस पुनर्वर्गीकरण से यह बदलाव आया कि इस अधिकार को कैसे लागू किया जा सकता है। जब यह मौलिक अधिकार था, तो कोई व्यक्ति इसके प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता था। संशोधन के बाद, संपत्ति का अधिकार केवल अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालयों के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार के प्रतिस्पर्धी हितों और सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति अर्जित करने की राज्य की आवश्यकता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाया गया था। इस प्रकार, इसे मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार में परिवर्तित करके, सरकार का उद्देश्य भूमि सुधार और संसाधनों के पुनर्वितरण सहित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपनी नीतियों को लागू करने में अधिक विवेक रखना है।
संपत्ति के अधिकार में किए गए संशोधनों पर न्यायिक रुख
अनुच्छेद 19(1)(f) और 31, जब अन्य अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाता है, तो वे अधिकार हैं जिन्हें संविधान में इस तरह से शामिल किया गया था कि उन्हें अधिकारों के पूरे ढांचे से बाहर नहीं किया जा सका। बिना किसी व्यवधान के इन अधिकारों को हटाना चुनौतीपूर्ण था। शेष संविधान के साथ सामंजस्य लाने के लिए, कमियों और व्यवधानों को संबोधित करने और सही करने की आवश्यकता है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, और अदालतों से कई बार कानून की सही स्थिति पर विचार करने के लिए कहा गया है, खासकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में कई संशोधन किए जाने के बाद।
सर्वोच्च न्यायालय ने, कई निर्णयों के माध्यम से, संशोधनों पर पुनर्विचार किया और उनके अभ्यास को तर्कसंगत मापदंडों तक सीमित कर दिया। कवलप्पारा कोट्टाराथिल कोचुनी बनाम मद्रास राज्य और अन्य (1960), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 31(1), संशोधन के बाद, किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनने के लिए राज्य को पूर्ण शक्ति प्रदान करने की मांग करता है। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31(1) और अनुच्छेद 31(2) दो अलग-अलग मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 31(1) में “कानून” शब्द का अर्थ वैध कानून है। अनुच्छेद 31 के अनुसार, इस कानून को अनुच्छेद 19(5) के प्रावधानों के तहत जनता के हित में एक उचित प्रतिबंध के रूप में योग्य होना चाहिए। जबकि निर्णय ने जहां आवश्यक हो, कानून द्वारा किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने की राज्य की शक्ति को मान्यता दी, इसने एक शर्त भी स्थापित की कि जिस कानून के तहत किसी व्यक्ति की संपत्ति ली जा सकती है वह उचित और जनता के हित में होना चाहिए और उसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है।
पी. वज्रवेलु मुदालियर बनाम स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, मद्रास और अन्य (1964) और भारत संघ बनाम मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य (1966) के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31(2) के तहत संपत्ति अधिग्रहण के लिए मुआवजे के पहलू का विश्लेषण किया। न्यायालय ने माना कि यदि मुआवज़ा निर्धारित करना काल्पनिक है या मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए लागू किए गए सिद्धांत अधिग्रहण के समय संपत्ति के मूल्य के लिए पर्याप्त नहीं थे, तो यह विधायी शक्तियों का दुरुपयोग होगा। परिणामस्वरूप, एक कानून के रूप में इसे अपर्याप्त और अमान्य माना जाएगा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ कानूनों और संबंधित मामलों की संवैधानिक चुनौती से निपटते हुए, आई. सी. गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1967) (इसके बाद इसे ‘गोलकनाथ मामले’ कहा जाएगा) के मामले में एक तीव्र रूप से विभाजित निर्णय (6:5) दिया। बहुमत के फैसले ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह मामलों में पहले के फैसलों को उलट दिया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि संवैधानिक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत बताए गए ‘कानून’ के अर्थों में शामिल हैं। इस प्रकार, इसमें कहा गया कि संसद संविधान में संशोधन करके बुनियादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उनमें से अधिकांश ने यह भी पाया कि संविधान ने पहले, चौथे और सत्रहवें संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे को सीमित कर दिया है। फिर भी, अदालत ने इन संशोधनों को जारी रखने की अनुमति दी क्योंकि उन्हें पिछले निर्णयों (जैसे शंकरी प्रसाद मामले) में कानूनी घोषित किया गया था और इन संशोधनों के आधार पर असंख्य राज्य कानून और संपत्ति अधिकार बनाए गए हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए, न्यायालय ने संभावित अधिनिर्णय की विधि को नियोजित किया, जिसका अर्थ है कि नए अर्थ को भविष्य के मामलों में लागू किया जाएगा, लेकिन कानून की पूर्व व्याख्याओं के आधार पर पूर्व संशोधनों और कार्यों को अमान्य नहीं माना जा सकता है।
केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्य (1973) (इसके बाद ‘केशवानंद भारती मामला’ के रूप में संदर्भित) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार में किए गए कुछ संवैधानिक संशोधनों की वैधता पर विचार किया। मामले का फैसला एक संकीर्ण रूप से विभाजित अदालत (7:6) द्वारा किया गया और गोलक नाथ मामले में अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13 के खंड (2) में ‘कानून’ शब्द में संवैधानिक संशोधन शामिल नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के खंड (2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से परे है। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि यद्यपि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति है, लेकिन उसके पास संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं है। इस कानूनी प्रस्ताव को बुनियादी संरचना सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा और यह भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र (ज्यूरिस्प्रूडेंस) का हिस्सा बन गया।
इस फैसले के बाद, संसद ने 44वां संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) को मौलिक अधिकारों की स्थिति से हटा दिया गया जो संविधान की मूल संरचना बनाते हैं। वामन राव और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1981), के बाद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले के आलोक में संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित संशोधनों और कानूनों पर चर्चा की। यह माना गया कि केशवानंद भारती मामले के फैसले से पहले नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित सभी संवैधानिक संशोधन और अधिनियम संरक्षित रहेंगे और उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, केशवानंद मामले में निर्णय के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी संशोधन और कानून को केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन माना गया था।
44वें संशोधन अधिनियम के बाद संपत्ति के अधिकार की स्थिति
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और संपत्ति के अधिकार के इतिहास से पता चलता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिए जाने के बावजूद, यह कानून के शासन द्वारा संरक्षित है। अदालतों के फैसलों में उभरते रुझान यह भी दर्शाते हैं कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और विशेष रूप से आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 300-A की भाषा महत्वपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 21 और 265 के साथ इसकी समानता दर्शाती है कि यह कानून के शासन के संरक्षक के रूप में कार्य करती है।
महाराव साहब श्री भीम सिंहजी बनाम भारत संघ (1980) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के मौलिक अधिकार के महत्व पर चर्चा की, भले ही इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया हो। इसके उन्मूलन के बावजूद, न्यायालय ने समानता के मौलिक अधिकार पर भरोसा करते हुए संपत्ति के अधिकारों के महत्व को स्वीकार किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता की अवधारणा पर आधारित है। इसलिए, अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता और समानता के परीक्षण को लागू करके, सर्वोच्च न्यायालय शहरी भूमि सीमा कानूनों के प्रावधानों को रद्द करने में सक्षम था, जो अनुचित थे। इस निर्णय ने स्थापित किया कि हालाँकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी इसे भारत के संविधान के तहत अन्य अधिकारों, विशेष रूप से समानता के अधिकार के उपयोग के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है।
2000 के दशक से विभिन्न कारणों से राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इस तरह के अधिग्रहण, मुख्य रूप से बांधों या उद्योगों के निर्माण के लिए, लाखों गरीब किसानों और पारंपरिक समुदायों जैसे कि स्वदेशी वनवासियों, मवेशी चराने वालों, मछुआरों और आदिवासी लोगों को हटाने का कारण बने हैं। वर्ष 2009 में, संजीव अग्रवाल बनाम भारत संघ (2009) रिट याचिका (सी) संख्या 464/2007 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने चौवालीसवें संवैधानिक संशोधन को रद्द करने और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना और नर्मदा बांध जैसी अन्य परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन (डिसप्लेसमेंट) के अलावा सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि “अधिग्रहण” आंदोलन को याचिकाकर्ता ने इस मांग का मुख्य कारण बताया। याचिकाकर्ता का तर्क कानूनी प्रतिनिधि द्वारा आई. आर. कोएल्हो (मृत) बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (2007) में दिए गए निर्णय पर आधारित था जिसमें यह माना गया कि मौलिक अधिकार संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा हैं और इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया था। चूँकि संपत्ति का अधिकार उस समय अनुच्छेद 19(1)(f) के तहत एक मौलिक अधिकार था, जब अदालत ने केशवानंद भारती मामले में अपना निर्णय सुनाया था, इसलिए, चौवालीसवें संशोधन के संचालन द्वारा इसे हटाने की बात कही गई थी संविधान की मूल संरचना को नकारना और इस प्रकार,असंवैधानिक था। हालाँकि, 2010 में, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की योग्यता पर ध्यान दिए बिना उसे खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता के पास जनहित याचिकाकर्ता के रूप में संशोधन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार के निरस्त होने के परिणामस्वरूप उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि याचिका पर विचार करने के लिए संपत्ति के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक मामले कानूनों पर फिर से विचार करना होगा।
हाल के वर्षों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत ‘सार्वजनिक उद्देश्य’ और ‘मुआवजे’ की आवश्यकताओं को दोहराया है। के.टी. प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य (2011), के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ‘कानून का शासन’ भारत में सर्वोच्च है और पाया कि जब किसी व्यक्ति को निजी उद्देश्य के लिए मुआवजे के साथ या उसके बिना उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है, तो न्यायालय शक्तिहीन नहीं है। इसलिए, जहां कोई राज्य संपत्ति अर्जित करता है, उसे अनुच्छेद 300A के तहत दिए गए ‘सार्वजनिक उद्देश्य’ और ‘मुआवजा’ दोनों प्रावधानों को पूरा करना होगा।

इसी तरह, सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड (2012), के मामले में अदालत ने बौद्धिक संपदा (इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के संबंध में ‘सार्वजनिक उद्देश्य’ और ‘मुआवजे’ की आवश्यकता को दोहराया। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 300A के तहत ‘कॉपीराइट’ को ‘संपत्ति’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 31 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधानों को वैध कानून की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए और सार्वजनिक हित में होना चाहिए। नारायण प्रसाद बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2017), में उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि भारत के संविधान के 300-A के अनुसार संपत्ति का अधिकार न केवल एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है बल्कि एक मानव अधिकार भी है। इसने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार केवल कानून में प्राधिकारी द्वारा ही छीना जा सकता है।
कानूनी प्रतिनिधि द्वारा बजरंग (मृत) बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के प्रावधानों को छुआ, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इस विशेष मामले में एक विवाद शामिल था जिसमें सरकार ने दावा किया था कि उसकी अतिरिक्त भूमि थी, हालाँकि वहाँ कोई अतिरिक्त भूमि नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हालांकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संरक्षित है। न्यायालय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार से कोई भी वंचित उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एकतरफा स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती या संपत्ति नहीं ले सकती। परिणामस्वरूप, चूंकि सरकार यह साबित करने में विफल रही कि जैसा कि उन्होंने प्रस्तावित किया था, अधिशेष (सरप्लस) भूमि थी, न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि सरकार के कार्य अनुचित थे।
इसके अलावा, रवींद्रन बनाम जिला कलेक्टर, वेल्लोर जिला (2020), के मामले में न्यायालय ने कानून के अधिकार को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि सरकार को किसी नागरिक के संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार तभी है जब यह कानून के अनुसार किया जाता है। इस मामले में दिए गए निर्णय को मद्रास उच्च न्यायालय ने जयलक्ष्मी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) के मामले में बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की कोई भी कार्रवाई जो किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को प्रभावित करती है, उसे जीवन के अधिकार से संबंधित व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों के भीतर स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति का अधिकार
44वें संशोधन अधिनियम के बाद, संपत्ति का अधिकार अब भारत के संविधान के भाग III में शामिल नहीं है। इस कारण से, कोई व्यक्ति जिसके अनुच्छेद 300-A के तहत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकता है। जिस उपाय के तहत वे लाभ उठा सकते हैं वह अनुच्छेद 226 के माध्यम से या सिविल अदालतों में है। प्रारंभ में, अनुच्छेद 31(1) में प्रावधान था कि कानून के प्राधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान को अनुच्छेद 300-A द्वारा प्रतिस्थापित और पुनः प्रकट किया गया, जिसमें कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए एक कानून की आवश्यकता है।
दुनिया का हर लोकतांत्रिक देश मानता है कि इससे पहले कि सरकार किसी के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करे या यह मांग करे कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे को दे दे, एक कानून होना चाहिए और वह कानून वैध होना चाहिए। संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने, कम करने या बदलने की क्षमता केवल विधायी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। इस प्रकार, कोई भी कार्यकारी कार्रवाई जो कानून की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करती है उसे संवैधानिक नहीं माना जा सकता है। अनुच्छेद 300-A में ‘कानून’ शब्द का अर्थ वैध कानून है। जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य (1994) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 300-A में ‘कानून’ का जिक्र करते समय, यह स्पष्ट कर दिया कि इसमें केवल संसद या किसी राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या एक कानूनी नियम या वैधानिक आदेश निहित है। यह व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि केवल वे कानून जो उचित विधायी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, या वैधानिक आदेश जिनमें कानून की ताकत है, अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कार्यों को उचित ठहरा सकते हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A की प्रयोज्यता
विजय महोबिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2022) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 300A के दायरे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई एकल न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बैंकों ने डीआरटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए उसे उस संपत्ति से गैरकानूनी तरीके से बेदखल करने की मांग की, जिस पर उसका कानूनी स्वामित्व था, जिसमें नीलामी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी गई थी। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप को रोकने के लिए निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के आदेश की मांग करते हुए पहले ही एक सिविल मुकदमे में अपना उपाय अपना लिया है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि मौजूदा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से ही सिविल मुकदमे के तहत इस उपाय की मांग कर रहा था। अनुच्छेद 300A की प्रयोज्यता पर चर्चा करते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 300A व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य के हाथ में एक हथियार भी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 300A का उपयोग किसी व्यक्ति के कार्यों के खिलाफ करने का इरादा नहीं है और ऐसी परिस्थितियों के लिए सिविल उपचार मौजूद हैं। अनुच्छेद 300A विशेष रूप से राज्य के हस्तक्षेप को रोकने के लिए बनाया गया है, खासकर उन मामलों में जहां जनता को लाभ पहुंचाने के लिए संपत्ति ली जाती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300-A की स्थिति को कोलकाता नगर निगम बनाम बिमान सिंह (2024) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से समझाया गया था जहां 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के साथ-साथ अनुच्छेद पर चर्चा की गई थी। अनुच्छेद 300-A में प्रावधान है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी को भी उसकी संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, निर्णय इस बात पर जोर देता है कि अनुच्छेद 300-A में ‘कानून का अधिकार’ वाक्यांश का अर्थ राज्य की अपने उपयोग के लिए भूमि लेने की शक्ति से परे है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कानून की प्रक्रियाएँ इस प्राधिकरण का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। उनका मतलब है कि संपत्ति का कोई भी अभाव कानूनी तरीकों से होना चाहिए और यह निश्चित रूप से वैध कानून के अनुसार होना चाहिए।
उपर्युक्त मामले में न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने बताया कि अनुच्छेद 300एlA में चुनौती का सामना राज्य द्वारा केवल एक ‘कानून’ होने से नहीं किया जा सकता है जो उसे संपत्ति लेने का अधिकार देता है। इसके लिए सख्त कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन की आवश्यकता होती है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान में निर्धारित उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करती है। इस तरह की व्याख्या यह गारंटी देने में मदद करती है कि राज्य कानूनी प्रक्रिया और कानून के शासन का पालन किए बिना किसी की संपत्ति नहीं छीन सकता है। इस मामले में, अदालत ने एक निजी व्यक्ति से संबंधित सात प्रक्रियात्मक अधिकारों की गणना की, जो परिभाषित करते हैं कि संपत्ति के अधिकार में क्या शामिल है और किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने से पहले राज्य को क्या कायम रखना चाहिए:
- नागरिकों को उनकी संपत्ति लेने के राज्य के इरादे के संबंध में नोटिस के माध्यम से सूचित किए जाने का अधिकार है।
- नागरिकों को सुने जाने का अधिकार है, जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य को अधिग्रहण के संबंध में नागरिकों की किसी भी आपत्ति पर ध्यान देना चाहिए।
- नागरिकों को अपनी संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में राज्य से तर्कसंगत निर्णय प्राप्त करने का अधिकार है।
- राज्य को यह साबित करना आवश्यक है कि अधिग्रहण सार्वजनिक उपयोग और हित के उद्देश्य से है।
- नागरिकों को राज्य से अपनी संपत्ति के लिए उचित मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है।
- राज्य को अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से और निर्धारित समयसीमा के अनुसार पूरा करना होगा।
- नागरिकों को अधिग्रहण प्रक्रिया के समापन का अधिकार है, जिसका अर्थ है राज्य द्वारा भूमि का भौतिक नियंत्रण लेना।
सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एसनरसिम्हा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से तभी पूर्ण होती है जब राज्य अधिग्रहीत भूमि पर भौतिक रूप से कब्ज़ा कर लेता है। इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-A के तहत संपत्ति के अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के दौरान नागरिकों की सुरक्षा की जाती है।

निष्कर्ष
भारत के संविधान के भाग III के तहत निहित मौलिक अधिकारों को किसी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। ऐसे अधिकारों में से एक है संपत्ति का अधिकार। विस्तृत चर्चा के बाद संविधान सभा ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। हालाँकि, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने के लिए कानून बना सकता है और ऐसे कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अन्य मौलिक अधिकारों को चुनौती दी गई है। किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार और सार्वजनिक कल्याण के लिए परियोजनाएं संचालित करने के राज्य के दायित्व के बीच विवाद के कारण ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से समाप्त कर दिया गया। इस तरह के निष्कासन के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए संपत्ति के अधिकार को एक आवश्यक अधिकार के रूप में बनाए रखने में हमेशा सुसंगत रहा है। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि संपत्ति का अधिकार, हालांकि मौलिक अधिकार नहीं है, केवल एक वैध कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन करके ही कम किया जा सकता है और इसे हमेशा कानून के शासन के सिद्धांतों पर सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत ‘व्यक्ति’ और ‘संपत्ति’ की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की प्रयोज्यता केवल भारत के नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गैर-नागरिकों तक भी है और ‘संपत्ति’ शब्द अपने आप में मूर्त और अमूर्त संपत्ति के साथ-साथ किसी भी हित को भी शामिल करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या पेंशन संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक संपत्ति है?
हाँ श्री नैनी गोपाल बनाम भारत संघ और अन्य (2020), के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को देय पेंशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक संपत्ति है, इसलिए राज्य द्वारा ऐसी संपत्ति से कोई भी वंचित कानून के अनुसार होना चाहिए। अदालत ने राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में कानून के शासन को कायम रखते हुए माना कि बैंक की कार्रवाई मनमाने, अनुचित, अनधिकृत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसमें पेंशन की सटीकता के बारे में पत्राचार करना या कटौती के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करना शामिल था। विश्वनाथ विश्वकर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (प्रधान सचिव राजस्व विभाग लखनऊ के माध्यम से) और अन्य (2023) के एक अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति माना जाता है और कानूनी अधिकार के बिना इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।
क्या अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार गैर-नागरिक को उपलब्ध है?
हाँ लखनऊ नगर निगम एवं अन्य बनाम कोहली ब्रदर्स कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (2024), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार उस व्यक्ति को भी उपलब्ध है जो भारत का नागरिक नहीं है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसमें ‘शत्रु संपत्ति’ की स्थिति से संबंधित मुद्दा शामिल था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत ‘लोगों’ और ‘संपत्ति’ की परिभाषाओं को स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते हुए ‘संपत्ति’ और ‘व्यक्ति’ शब्दों के अर्थ का विस्तार करते हुए कहा कि “अनुच्छेद 300A में ‘व्यक्ति’ शब्द में न केवल कानूनी या न्यायिक व्यक्ति बल्कि भारत के गैर-नागरिक भी शामिल हैं। ‘संपत्ति’ शब्द व्यापक है, इसमें मूर्त और अमूर्त संपत्ति, साथ ही संपत्ति में सभी अधिकार, शीर्षक और हित शामिल हैं। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 300A में इस्तेमाल किया गया ‘व्यक्ति’ शब्द भारतीय नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी संरक्षक द्वारा रखी गई संपत्ति किसी शत्रु से हस्तांतरित की जाती है, तो वास्तविक मालिक, भले ही वह शत्रु ही क्यों न हो, के पास स्वामित्व का अधिकार होता है। जब ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है तो उन्हें संपत्ति के मालिक को मुआवजा देना होगा।
संपत्ति का क्या अर्थ है?
सामान्य उपयोग में, संपत्ति का अर्थ ऐसी कोई भी चीज़ है जो किसी व्यक्ति की हो या जिसका स्वामित्व उसके पास हो। ऐसी संपत्तियों के उदाहरण मूर्त संपत्ति जैसे भूमि, भवन और अन्य व्यक्तिगत संपत्ति, या अमूर्त संपत्ति जैसे बौद्धिक संपदा और डिजिटल संपत्ति, अन्य हो सकते हैं। संपत्ति को अंग्रेजी में ‘प्रॉपर्टी’ कहा जाता है इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ‘प्रोप्रिएटस’ से हुई है जिसका अर्थ किसी चीज़ का मालिक होना है, है। यह शब्द किसी चीज़ के मालिक होने और उस पर कब्ज़ा करने के बीच के संबंध पर प्रकाश डालता है। संपत्ति और स्वामित्व को संबंधित अवधारणाएं माना जा सकता है, स्वामित्व का तात्पर्य संपत्ति की किसी वस्तु के कानूनी अधिकार या शीर्षक से है। आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (1970), के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी ढांचे के भीतर संपत्ति की अवधारणा की व्याख्या की। अदालत ने कहा कि “संपत्ति” में भूमि और फर्नीचर जैसी मूर्त वस्तुएं और कॉपीराइट और पेटेंट जैसी अमूर्त वस्तुएं दोनों शामिल हैं। हालाँकि, न्यायालय का हालिया दृष्टिकोण बदल गया है। यह अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में संपत्ति पर विचार करता है, यह मानते हुए कि स्वामित्व वाली संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रताएं भी इस प्रावधान के तहत मौजूद हैं।
मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार के बीच क्या अंतर है?
जबकि मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों भारतीय संविधान में निहित हैं, दिए गए अधिकारों, दी गई सुरक्षा की डिग्री और इन अधिकारों को किस हद तक लागू किया जा सकता है, के संदर्भ में अंतर हैं। संविधान के भाग III के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्हें मौलिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि भाग III के तहत निर्दिष्ट अधिकारों को किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इन अधिकारों में समानता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और दूसरों के बीच भेदभाव से सुरक्षा शामिल है। मौलिक अधिकार सीधे न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति इन अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इन अधिकारों में संशोधन करना अधिक कठिन है क्योंकि संसद केवल संविधान की मूल संरचना को बदले बिना ही इनमें संशोधन कर सकती है जैसा कि केशवानंद भारती के मामले में हुआ था। इसके अलावा, संविधान के भाग III के तहत प्रदान किए गए कुछ अधिकारों को आपातकाल की स्थिति के दौरान प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने की स्वतंत्रता भी शामिल है।
दूसरी ओर संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के संविधान के तहत भी प्रदान किए गए हैं, हालांकि उन्हें भाग III के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। वे संविधान के अन्य भागों में शामिल हैं और सुरक्षा की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, उदाहरण के लिए संपत्ति का अधिकार, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत प्रदान किया गया है। ये अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित हैं लेकिन इन्हें मौलिक अधिकारों जितना आवश्यक नहीं माना जाता है। जबकि संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं और न्यायपालिका के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं, आमतौर पर एक अलग प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, जो अक्सर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के माध्यम से होता है। मौलिक अधिकारों की तुलना में इन्हें संसद द्वारा बदलना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि ये संविधान के मूल संरचना सिद्धांत द्वारा संरक्षित मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आते हैं। सामान्य तौर पर, आपातकाल की स्थिति के दौरान संवैधानिक सुरक्षा को निरस्त नहीं किया जाता है जब तक कि राज्य अन्यथा प्रदान नहीं करता है।
संविधान सभा ने भारतीय संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्यों जोड़ा?
संविधान सभा ने एक ऐसी कानूनी प्रणाली की कल्पना की जो लोकतांत्रिक समाजवाद और उदार लोकतंत्र का एक अनूठा मिश्रण थी। इस प्रणाली से अपेक्षा की गई थी कि यह भूमि सुधार और संसाधन वितरण सहित सामाजिक और आर्थिक सुधार की दिशा में काम करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगी। हालाँकि, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और अधिक न्यायसंगत समाज बनाने के उद्देश्य से भूमि पुनर्वितरण पर नीति शुरू करने के बीच विवाद था। इससे संविधान सभा के भीतर बहस शुरू हुई और अंततः, इन दो प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित हुआ। परिणामस्वरूप, भारत के संविधान के भाग III के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को अपनाया गया।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में डालने का क्या मतलब है?
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में बदलने का मतलब है कि सुरक्षा का स्तर और साथ ही इस अधिकार का उल्लंघन होने पर प्रभावित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध उपचार बदल गए हैं। मौलिक अधिकार के रूप में, संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के भाग III के तहत उच्च सुरक्षा प्राप्त है, जिससे व्यक्तियों को अनुच्छेद 32 के तहत उल्लंघनों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति मिलती है, जिससे मजबूत और तत्काल प्रवर्तन सुनिश्चित होता है। संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप करने से पहले राज्य को कड़े मानकों और अदालतों की जांच का सामना करना पड़ा। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में, इस अधिकार के किसी भी उल्लंघन को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जानी है। इसका मतलब यह है कि राज्य को सार्वजनिक हितों के लिए संपत्ति को जब्त करने की अपनी शक्ति को विनियमित करने या यहां तक कि प्रयोग करने के मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक छूट प्राप्त है।
स्वतंत्रता-पूर्व भारत में संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या थी?
स्वतंत्रता-पूर्व परिदृश्य में, संपत्ति के स्वामित्व और निपटान के संबंध में प्रासंगिक प्रावधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मौजूद थे, जिसे एक दमनकारी कानून माना जाता था। अधिक विशेष रूप से, उपरोक्त अधिनियम की धारा 299 ने सभी वर्गों के लोगों, जमींदारों और किसानों दोनों को संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की। इस धारा ने यह सुनिश्चित किया कि उचित मुआवजे के बिना लोगों की संपत्ति का शोषण या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने संपत्ति मालिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की और माना कि सरकार केवल जनता के हित में व्यक्तियों से संपत्ति प्राप्त कर सकती है। यह सुरक्षा महत्वपूर्ण थी ताकि मालिकों से अनुचित तरीके से संपत्ति न छीनी जा सके और यदि ऐसा था, तो इसे निष्पक्ष और सही तरीके से किया जाना चाहिए।
संदर्भ