यह लेख Soumya Lenka द्वारा लिखा गया है। यह किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु मामले की पृष्ठभूमि, प्रासंगिक तथ्यों, पक्षों की दलीलों और फ़ैसला सुनाने के पीछे अदालत के तर्क से संबंधित है। यह मामला संविधान (बावनवाँ) संशोधन अधिनियम, 1985 जिसने दसवीं अनुसूची पेश की थी, की वैधता पर चर्चा करते हुए, मुख्य रूप से दलबदल विरोधी (एंटी डिफेक्शन) कानून से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लु और अन्य (1993) का मामला दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है। “दलबदल” शब्द किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा विद्रोह, असहमति और बगावत को इंगित करता है। आम तौर पर, दलबदल का मतलब किसी संगठन को छोड़कर दूसरे संगठन में शामिल होना होता है। राजनीतिक परिदृश्य में, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों से हाथ मिला लेता है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में इस बुरी घटना में भारी उछाल आया। एक समय ऐसा आया जब देश में दलबदल विरोधी कानून होना ज़रूरी हो गया और हमारे विधायकों ने इस मुद्दे से निपटने के लिए एक अनुसूची बनाई। इस मामले को एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है क्योंकि यह भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता पर प्रकाश डालता है, जिसे संविधान (बावनवां) संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से पेश किया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
जब संस्थापक पिता देश के सबसे पवित्र ग्रंथ या आधारभूत मानदंड, यानी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भारतीय राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ ऐसे मुद्दों का सामना करना पड़ेगा, जिनसे निपटने के लिए वर्तमान संविधान पूरी तरह से सक्षम नहीं होगा। इससे निपटने के लिए, उन्होंने अनुच्छेद 368 (संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उस पर प्रक्रिया) के रूप में संशोधन का प्रावधान किया।
जब हमारा संविधान तैयार किया गया था, तब भारतीय राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में देश के बुद्धिजीवियों का एक समूह शामिल था, और वे उच्च राजनीतिक नैतिकता और अनुशासन रखते थे। हालाँकि, धीरे-धीरे, जैसे-जैसे साल बीतते गए, नैतिकता ने करवट ली, और राजनीतिक व्यवस्था, असामाजिक तत्वों और सत्ता के भूखे लोगों से भर गई।
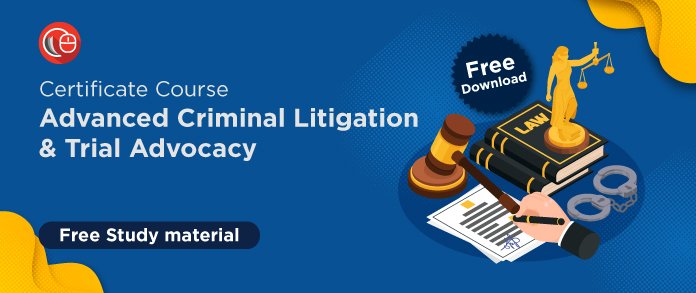
भारतीय राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बुरी प्रथाओं में से एक दलबदल की प्रथा थी। दलबदल का मतलब आम तौर पर विद्रोह या असहमति होता है। भारतीय राजनीतिक संदर्भ में, इसका मतलब है कि राज्य विधानमंडल या संसद के सदस्य द्वारा विधानमंडल में चुने जाने के बाद कई नापाक और बुरे कारणों से राजनीतिक दल बदलना।
यह घटना ब्रिटिश विधानमंडल में फ्लोर क्रॉसिंग से जुड़ी है, जिसमें एक सदस्य पिछली पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधानमंडल में चुने जाने के बाद अपना राजनीतिक संगठन बदल लेता है और पार्टी बदल लेता है। यह घटना 1960, 1970 और 1980 के दशक के अंत में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक रूप से प्रचलित हुई।
इसका सबसे चर्चित उदाहरण हरियाणा के एक विधानसभा सदस्य गयालाल का प्रसिद्ध मामला है। हरियाणा राज्य ने 1967 में अपना पहला विधानसभा चुनाव देखा। गयालाल नामक एक स्वतंत्र उम्मीदवार नवगठित 81 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। चुने जाने के कुछ ही घंटों के भीतर वे कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके कुछ ही घंटों के भीतर वे संयुक्त मोर्चा गठबंधन में चले गए और फिर अगले कुछ घंटों के भीतर वे वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आए।
यह एक अजीबोगरीब मामला था। उन्होंने एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदली। उनके साथी कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, “गया राम अब आया राम है”। मीडिया ने इस मुहावरे का एक बदला हुआ संस्करण लिया और “आया राम गया राम” का इस्तेमाल किया, जो इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी भारतीय राजनीति में इसका इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब कोई राजनेता जो किसी राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होता है या संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है, पार्टी बदलता है (दलबदल करता है)। गया राम की तरह ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और अब समय आ गया है कि भारत में इस राजनीतिक दंड से बचने के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया जाए।
दिसंबर 1967 में, लोकसभा के एक निजी सदस्य ने इस ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करते हुए एक विधेयक पेश किया। विधेयक के अनुसरण में, भारत के तत्कालीन गृह मंत्री वाईबी चव्हाण की अध्यक्षता में दलबदल पर एक समिति गठित की गई। वाईबी चव्हाण समिति ने सुझावों की एक सूची बनाई, जिसे फरवरी 1969 में संसद में प्रस्तुत किया गया। दुर्भाग्य से, समिति के सुझाव समस्या का समाधान नहीं दे सके।
वाईबी चव्हाण रिपोर्ट और उसकी विफलता के बाद, दो ऐसे मौके आए जब सरकार ने दलबदल विरोधी मुद्दे को संबोधित करने के लिए कानून पेश करने की कोशिश की। एक 1973 में था, और दूसरा 1978 में। हालांकि, दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि दोनों विधेयक संसद के दोनों सदनों में आम सहमति बनाने में विफल रहे, और किसी न किसी कारण से, ये विधेयक कभी पारित नहीं हो पाए। भारतीय राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में दलबदल विरोधी कानून पेश करने के दोनों प्रयास विफल रहे।
अंत में, 1985 में, 52वां संशोधन अधिनियम, जो दलबदल विरोधी तंत्र प्रदान करता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 (जिसे दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है) के माध्यम से भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची डाली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 101 की (संसद के संबंध में सीटों की रिक्ति), 102 (संसद के संबंध में सदस्यता के लिए अयोग्यता), 190 (राज्य विधानसभाओं के संबंध में सीटों की रिक्ति) और 191 (राज्य विधानसभाओं के संबंध में सदस्यता के लिए अयोग्यता) में परिवर्तन करके दलबदल के आधार पर संसद के दोनों सदनों या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया था।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु
- याचिकाकर्ता: किहोतो होलोहान
- उत्तरदाता: ज़ाचिल्लू और अन्य
- मामले का प्रकार: स्थानांतरण याचिका (दीवानी)
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- पीठ: न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा, एमएन वेंकटचलैया, जेएस वर्मा, के. जयचंद्र रेड्डी और एससी अग्रवाल
- फैसले की तारीख: 18. 02. 1992
- उद्धरण (साइटेशन): एआईआर 1993 SC 4120
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1993) में चर्चित कानून
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची
मुख्य रूप से, यह मामला दसवीं अनुसूची और संघ द्वारा शुरू किए गए दलबदल विरोधी कानून के इर्द-गिर्द घूमता है। सबसे पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में दलबदल का क्या मतलब है। दलबदल का मतलब है विधायिका के सदस्य की राजनीतिक संबद्धता में परिवर्तन, जो आम तौर पर किसी नापाक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए होता है। दसवीं अनुसूची भारतीय संसद द्वारा 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से दलबदल की बढ़ती प्रवृत्ति और राजनीतिक संकट को रोकने के लिए लाई गई थी, जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बढ़ रही थी। दसवीं अनुसूची में कई आधारों पर राज्य और संघ विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं। इस अनुसूची की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –
- यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है, तो वह सदस्य विधानमंडल से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का सदस्य होते हुए, उस राजनीतिक दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मतदान से दूर रहता है या उस राजनीतिक दल के निर्देश के विरोध में वोट देता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- यदि सदन का कोई स्वतंत्र सदस्य, अर्थात् कोई ऐसा व्यक्ति जिसका किसी राजनीतिक संबद्धता नहीं है, को निर्वाचक मंडल द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में चुना गया है, तो वह विधानमंडल द्वारा अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यदि वह राज्य या संघ विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- मनोनीत सदस्यों के मामले में, दसवीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि यदि वह संबंधित राज्य विधानसभा या संसद के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह माह की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है या राजनीतिक संबद्धता बदलता है तो वह अयोग्य हो जाएगा।
मामले के तथ्य
हाल ही में शुरू किए गए दलबदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दलों में व्यापक हलचल मचा दी थी और उस समय यह गरमागरम बहस का विषय था। यह मामला 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के बाद की स्थिति पर आधारित है। विवादास्पद संशोधन के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाएँ दायर कीं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न रिट याचिकाओं, स्थानांतरण याचिकाओं, सिविल अपीलों, विशेष अनुमति याचिकाओं और अन्य संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए एक साथ रखा क्योंकि वे समान विषय वस्तु से संबंधित थे। चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि दलबदल विरोधी कानून और विशेष रूप से दसवीं अनुसूची संवैधानिक योजना और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और इसलिए इसे रद्द करने की आवश्यकता है। दलबदल विरोधी कानून के इर्द-गिर्द चिंता के कई पहलू थे।
- दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 7 संविधान के भाग V के अध्याय IV और भाग VI के अध्याय V का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति), सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति) और अनुच्छेद 227 (उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति) के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को छीन लेता है।
- राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले विधेयक को अनुच्छेद 368(2) की योजना के अनुसार, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालाँकि, संबंधित कानून को ऐसे किसी भी अनुमोदन से नहीं गुज़ारा गया।
- दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 7 न्यायिक समीक्षा (रिव्यू) की शक्ति को छीन लेता है या उसे कमजोर कर देता है क्योंकि यह लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष (चेयरमैन) के निर्णय को दलबदल और उसके बाद विधानसभाओं के संबंधित सदस्यों की अयोग्यता के मामले में बाध्यकारी बनाता है, इस प्रकार वह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। और चूंकि न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान की एक बुनियादी और मौलिक संरचना है, इसलिए यह योजना इसके विपरीत है, और इसलिए संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।
- दल-बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने की अवधारणा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय लोकतंत्र में प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत के विपरीत है तथा भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल है।
- नए दलबदल विरोधी कानून के कारण निर्वाचित सदस्य के असहमति के अधिकार, चुनाव करने के अधिकार तथा अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लग गया है।
- दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(b) में “किसी निर्देश” वाक्यांश का प्रयोग स्पष्टतः अस्पष्ट और भ्रामक है, और यह अध्यक्ष के हाथों में कोई भी निर्देश जारी करने के लिए अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान करता है।
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1993) में उठाए गए मुद्दे
विवादित मामले में निर्णय हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे रखे गए:
- क्या संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई दसवीं अनुसूची संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों और भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है?
- क्या नव सम्मिलित दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 227 में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और भारतीय न्यायपालिका की पूर्ण शक्तियों में हस्तक्षेप हुआ है?
- क्या अनुच्छेद 7 को अनुच्छेद 368(2) में निहित योजना के अनुसार आधे राज्यों के राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है?
- क्या अनुच्छेद 368(2) के तहत परिकल्पित योजना का अनुपालन न करने से संपूर्ण संशोधन अमान्य हो जाएगा और संशोधन अधिनियम को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा कि यह भारतीय संविधान की योजना को निरस्त करने का विधायिका और सरकार का असफल प्रयास है?
- क्या पृथक्करण के सिद्धांत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका द्वारा दसवीं अनुसूची के केवल पैराग्राफ 7 को ही निरस्त किया जाना है?
- क्या दसवीं अनुसूची ने ऐसी योजना या न्यायिक प्रक्रिया बनाई है जो न्यायपालिका को न्यायिक तंत्र के रूप में कार्य करने से रोकती है, अर्थात यह दलबदल के आधार पर अयोग्यता के मामलों में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायिक समीक्षा से वर्जित कर देती है?
- क्या दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 6(1) सदस्यों की अयोग्यता के मामले में अध्यक्ष के निर्णय को अंतिमता प्रदान करके न्यायिक समीक्षा के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और असंवैधानिक है?
- क्या न्यायिक तंत्र, जिसमें अध्यक्ष शामिल होता है, संसदीय लोकतंत्र में विधि के शासन के निष्पक्ष सिद्धांत के अनुरूप है, जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में परिकल्पित है, तथा क्या यह न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने की सीमा तक समानांतर न्यायिक तंत्र के रूप में खड़ा हो सकता है?
पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वकील श्री एफ.एस. नरीमन, श्री शांति भूषण, श्री एम.सी. भंडारे, श्री कपिल सिब्बल, श्री शर्मा, श्री भीम सिंह और श्री राम जेठमलानी ने किया था।

यह तर्क दिया गया कि 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संघ विधानमंडल द्वारा डाली गई दसवीं अनुसूची स्पष्ट रूप से मनमानी है। यह कहा गया कि यह संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है, भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित मूल सिद्धांतों के विपरीत है, और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। दसवीं अनुसूची मूल रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति के अधिकार और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करती है, जो एक स्वस्थ, कार्यशील लोकतंत्र के मूल में निहित हैं।
रोग को उपचार की आवश्यकता होती है, लेकिन जब उपचार रोग की आवश्यकता से अधिक हो, तो वह अपने आप में एक नया रोग बन जाता है। दूसरी पार्टी में जाना एक समस्या है, लेकिन दसवीं अनुसूची में इसके लिए निर्धारित उपचार स्वयं समस्या से कहीं अधिक बड़ा मुद्दा है। अपनी पार्टी की निष्ठा बदलने का निर्णय प्रतिनिधि के विवेक पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इस सादृश्य का सहारा लेकर यह तर्क दिया गया कि बुरे और नापाक इरादों से दलबदल की जांच की जानी चाहिए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्रवाई या उपाय निर्वाचित सदस्य के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में बाधा न बने और असहमति के अधिकार, जो भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं, का उल्लंघन न हो।
इस मामले में केंद्र सरकार ने दसवीं अनुसूची को लागू करके एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जो इतनी सख्त और मनमानी है कि यह न केवल दलबदल को एक घटना के रूप में प्रभावित करती है बल्कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के विवेक और पसंद की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर भी अंकुश लगाती है। इसलिए, दसवीं अनुसूची की योजना दलबदल की समस्या की मांग को खत्म कर देती है और अपने आप में एक बीमारी बन सकती है।
वकीलों ने एमाल्गमेटेड सोसाइटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स बनाम ओसबोर्न (1910) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि एक योजना (नए पेश किए गए दसवीं अनुसूची के तहत परिकल्पित योजना का जिक्र करते हुए) जो निर्वाचित सदस्य के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार, पसंद की स्वतंत्रता और विवेक के विपरीत है, वह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है। यह कहा गया कि संसदीय लोकतंत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि का अपने लोगों के प्रति सबसे महत्वपूर्ण दायित्व उनके अधिकारों और हितों और उन वादों को सही ठहराना है जो प्रतिनिधि ने चुने जाने के दौरान उनसे किए थे।
यदि वह जिस संसदीय या क्षेत्रीय (राज्य) दल से संबंधित है उसकी राय निर्वाचित सदस्य की राय से भिन्न है और निर्वाचित सदस्य सोचता है कि विचारों के कारण अपना राजनीतिक दल बदलना उसके आदर्शों और उन लोगों के अधिकारों और हितों के हित में होगा जिनके लिए वह खड़ा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोके। यह विकल्प भारतीय संविधान की संवैधानिक योजना में निहित है और इसे कानून की मंजूरी प्राप्त है। बिना किसी वैध आधार के इसे वापस लेना स्पष्ट रूप से मनमाना और असंवैधानिक है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक स्वतंत्र मतदाता द्वारा चुना जाता है। यह मतदाता एक चुनाव के लिए एक उम्मीदवार और दूसरे के लिए किसी अन्य उम्मीदवार को चुन सकता है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र जिस स्वतंत्रता का समर्थन करता है, उसके अनुसार यह तर्क दिया गया कि यदि चीजों को दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो निर्वाचित प्रतिनिधि भी अपने मतदाताओं के प्रति अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए और अपने राजनीतिक संघ या दल को बदलते हुए जैसा उचित समझे, वैसा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है।
यह भी कहा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105(2), जो संसद के निर्वाचित सदस्य को अधिकार और प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) प्रदान करता है, पूर्ण है और किसी भी कानून द्वारा इसकी जांच या रोकथाम नहीं की जा सकती। न्यायिक निर्णयों के आधार पर संघ के विधायकों को अनुच्छेद 105(2) द्वारा प्रदान की गई पूर्ण छूट संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत परिकल्पित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बेहतर है, और इसलिए विधायिका या केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने और कोई भी बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि विवादित दलबदल कानून पहली नज़र में असंवैधानिक है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि दसवीं अनुसूची के तहत दिए गए “दलबदल” और “विभाजन” शब्दों के बीच का अंतर इतना पतला और अस्पष्ट है कि यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि क़ानून क्या प्रदान करना या कहना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा अस्पष्ट प्रावधान उस उद्देश्य को पराजित करता है जिसके लिए कानून बनाया गया था और व्यापक अर्थों में, यह तर्कसंगतता और तर्क के सिद्धांतों की सख्त अवहेलना है, जिसके लिए कानून का शासन खड़ा है। आगे यह तर्क दिया गया कि यदि किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा पार्टी बदलना या राजनीतिक निष्ठा रखना कानून की नज़र में गलत और बुरा है, तो कानून के अनुसार, एक पार्टी के 1/3 सदस्यों का दूसरी पार्टी में जाना भी कम बुरा नहीं है और इसकी भी इसी तरह आलोचना की जानी चाहिए। हालांकि, दसवीं अनुसूची द्वारा परिकल्पित दलबदल विरोधी कानून और योजना में यह प्रावधान था कि पूर्व बुराई संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, लेकिन जब सामूहिक तैयारी की जाती है, जो कि बाद के मामले में होता है, तो इसे कानून की मंजूरी मिल जाती है और यह आलोचना के अधीन नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यह वर्गीकरण तर्क और औचित्य से रहित है, और जो कानून तर्क से रहित है वह स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
एच.एच. महाराजाधिराज माधव राव जीवाजी राव सिंधिया बहादुर एवं अन्य बनाम भारत संघ (1971) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा प्रदान किए गए संशोधन से अनुच्छेद 136, 226 और 227 की प्रकृति में परिवर्तन होता है तथा भारतीय न्यायपालिका की शक्ति में हस्तक्षेप होता है, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत प्रदान की गई योजना के अनुसार, इसे कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि विवादित परिदृश्य में है, योजना का पालन नहीं किया गया है, तथा संसद और केंद्र सरकार ने एकतरफा कानून पारित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि यह कानून असंवैधानिक है तथा इसमें कानून की स्वीकृति नहीं है।
यह भी तर्क दिया गया कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(b), 6(1), और 6(2) अध्यक्ष के हाथों में व्यापक शक्तियां देते हैं और उन्हें निर्वाचित सदस्यों के दलबदल से संबंधित मामलों के संबंध में एकमात्र न्यायनिर्णय प्राधिकारी बनाते हैं। अध्यक्ष को दी गई पूर्ण शक्तियों के अतिरिक्त, विशिष्ट तथ्य अयोग्यता कार्यवाही के मामलों में उनके निर्णय को अंतिमता प्रदान करते हैं। यह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह तर्क दिया गया कि न्याय के गढ़ के रूप में कार्य करने वाला एकमात्र प्राधिकरण या संस्थान भारतीय न्यायपालिका है, जो न्यायनिर्णय का सर्वोच्च प्राधिकारी है। इसलिए भले ही किसी प्राधिकारी के पास न्यायनिर्णय शक्तियां हों, लेकिन भारतीय न्यायपालिका का अंतिम कहना होगा या वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम सहारा होगी जो व्यथित है या निचले प्राधिकारियों के निर्णय से खुश नहीं है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को एक बुनियादी और मौलिक विशेषता के रूप में स्वीकार करती है, और विवादित मामलों में अध्यक्ष के निर्णय को बाध्यकारी बनाकर, विधायिका ने बुनियादी सिद्धांत को दरकिनार करने की कोशिश की है, और इसलिए, कानून को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण को किसी भी अनुचित प्रभाव या दबाव से मुक्त होना चाहिए। यदि अध्यक्ष को न्यायिक अधिकार दिया जाता है, जैसा कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में किया गया है, तो वह कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। यह तर्क दिया गया कि सदन का अध्यक्ष बने रहने के लिए, उसे सदन के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता होती है, और फिर भी यह उसके निर्णय लेने में पक्षपात की ओर ले जाता है, और इसलिए वह एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की बुनियादी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और कानून के शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
प्रतिवादी
विद्वान महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) श्री सोली जे. सोराबजी, श्री आर.के. गर्ग और श्री संतोष हेगड़े ने राज्य के पक्ष में तर्क दिया तथा संशोधन और दसवीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता का समर्थन किया।
संशोधन के पक्ष में प्रतिवादियों ने आग्रह किया कि दलबदल विरोधी एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा है और यह बहुत जरूरी है कि सरकार इस संबंध में कानून लाकर इसका समाधान करे। सरकार ने 52वां संशोधन अधिनियम, 1985 पारित किया और देश भर में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाले उभरते मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से दसवीं अनुसूची डाली। चूंकि यह एक जटिल राजनीतिक मुद्दा है और यह पूरी तरह से विधायी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए सरकार ने उचित रूप से इस मामले को न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया है और अध्यक्ष के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी बना दिया है।
इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि पूरी कार्यवाही को संसद या राज्यों के विधानमंडल के सदनों के भीतर की कार्यवाही मानकर, जैसा कि अनुच्छेद 122 (संसद की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जानी चाहिए) और अनुच्छेद 212 (राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जानी चाहिए) में परिकल्पित है, और साथ ही पैराग्राफ 7 के तहत न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर करके, विधायिका ने अयोग्यता कार्यवाही के लिए न्यायिक समीक्षा को उचित रूप से रोक दिया है। इसलिए, विधायिका ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कानून के दायरे में है।
राज्य की ओर से उपस्थित प्रतिवादियों द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि “रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है”। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों की दलीलों का विरोध करते हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दसवीं अनुसूची के प्रावधान दलबदल की समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत अधिक कठोर और सख्त हैं। हालांकि, यह तर्क दिया गया कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है, और विधायिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है और रोकथाम को ध्यान में रखते हुए दलबदल की समस्या से अधिक कठोर कानून बनाया है। यह तर्क दिया गया कि विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने की क्षमता और क्षमता है, और विधायी क्षमता के पहलू पर गहराई से विचार करना न्यायिक जांच के दायरे से बाहर है।

यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 368(2) और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा कहीं भी विवादित प्रकृति के किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को अनुमोदित करने का आदेश नहीं देती है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि संशोधन विधेयक पारित करते समय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है, किसी भी तरह से निराधार है।
किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हु (1993) में निर्णय
न्यायालय ने बहुमत के निर्णय (3:2 के अनुपात) में माना कि विवादित मामले में संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के दायरे में नहीं आता है, और अनिवार्य भाषा [इसके बाद संविधान संशोधित माना जाएगा] विवादित परिदृश्य में लागू नहीं होती है। इसलिए, राज्य विधानसभाओं या संसद द्वारा किसी भी अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार इस तरह के कानून को पारित करते समय कानून की सीमाओं के भीतर थी।
फैसले के पीछे तर्क
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1964) और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) के मामलों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी कि संपूर्ण दसवीं अनुसूची का अनुमोदन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इस तर्क पर आते हुए कि संपूर्ण दसवीं अनुसूची का अनुमोदन संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत प्रदान की गई योजना के अनुसार किया जाना चाहिए, माना कि सार और तत्व के सिद्धांत के अनुसार, अनुच्छेद 136, 226 और 227 के प्रावधानों की योजना की भाषा में विवादित अनुसूची द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस तर्क को नकारते हुए, न्यायालय ने माना कि सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद मामलों में दिए गए तर्क विवादित मामले में लागू नहीं होते हैं।
दसवीं अनुसूची के विवादास्पद पैराग्राफ 7 पर आते हुए, न्यायालय ने माना कि पैराग्राफ 7 निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136, 226 और 227 की योजना को बदलने का प्रयास करता है और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाधित करता है। इसलिए, इसे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत प्रावधान किया गया है। न्यायालय ने माना कि संपूर्ण दसवीं अनुसूची को असंवैधानिक घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। श्री केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य (1973) और मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1981) में परिकल्पित सिद्धांत पर भरोसा करते हुए कि केवल आपत्तिजनक भाग को अलग करने की आवश्यकता है, न्यायालय ने निर्णय लिया कि पृथक्करण के सिद्धांत का उपयोग करके केवल पैराग्राफ 7 को अलग करने की आवश्यकता है।
दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 की बात करें तो न्यायालय का मानना है कि संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष का पद सम्माननीय है। संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष को निष्पक्षता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है और संसदीय कार्यवाही के अनुशासन और संचालन के लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार होता है। सदन के कई महत्वपूर्ण कार्य उसके जिम्मे होते हैं और उनमें से कई न्यायिक प्रकृति के होते हैं। वह सदनों को उनके संबंधित नियमों के अनुसार चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। यही बात राज्यों की विधानसभाओं पर भी लागू होती है।
न्यायालय ने माना कि भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में अध्यक्ष के पद को धारण करने वाली प्रतिष्ठित संस्था को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष के निर्णय पर अविश्वास रखना हर दृष्टि से अनुचित है। केवल इसलिए कि ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य किया है, इससे याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का सामान्यीकरण नहीं हो सकता है कि अध्यक्ष का कार्यालय पक्षपातपूर्ण है और वह निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता कार्यवाही के मामलों में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अध्यक्ष के कार्यालय के खराब कामकाज के एकतरफा उदाहरणों को इस आरोप को पुष्ट करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है कि अध्यक्ष के पद में निर्णायक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने की क्षमता का अभाव है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के आरोपों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने दृढ़ता से माना कि दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 6 संवैधानिक रूप से वैध है और अध्यक्ष के पास ऐसे मामलों पर निर्णय लेने की विधायी क्षमता है।
अनुच्छेद 105(2) के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को पूर्ण उन्मुक्ति (इम्यूनिटी) दिए जाने के याचिकाकर्ताओं के तर्कों को नकारते हुए न्यायालय ने माना कि निर्वाचित सदस्यों को मानहानिकारक बयानों के मामलों में एक तरह की उन्मुक्ति प्रदान किए जाने के बावजूद, यह कहना कि यह पूर्ण है, केवल मूर्खता है। न्यायालय ने माना कि संसद और विधान सभाओं के सदस्यों को किसी भी रिपोर्ट, वोट, पेपर या संसदीय कार्यवाही के मामले में अदालती कार्यवाही से उन्मुक्ति दी जाती है, लेकिन यह सिद्धांतहीन फ्लोर क्रॉसिंग के परिदृश्य पर कहीं भी लागू नहीं होता है।
ज्योति बसु एवं अन्य बनाम देबी घोषाल (1982) पर भरोसा करते हुए न्यायालय का मानना था कि चुनाव का अधिकार, लोकतंत्र के लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक वैधानिक अधिकार है। इसी तरह से चुने जाने का अधिकार और चुनाव को चुनौती देने का अधिकार भी एक ही पायदान पर है। चूंकि यह एक वैधानिक अधिकार है, इसलिए यह वैधानिक सीमाओं और मानकों के अधीन भी है। इसलिए, वैधानिक विनियमन और कानून के माध्यम से इसकी शुद्धता सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है।
संसद को चुनावों की आदरणीय प्रक्रिया की रक्षा करने और चुनावी जनादेश को इस तरह दूषित होने से रोकने के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है जो देश के संसदीय लोकतंत्र की पवित्रता को कमजोर करता है। इसलिए न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) को इस कथन के अनुरूप पढ़ने पर कि चुनाव का अधिकार मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है, यह अच्छी तरह से स्थापित किया जा सकता है कि अनुच्छेद 105(2) निरपेक्ष नहीं है और वैधानिक नियमों के अधीन है। इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने फैसला किया कि दसवीं अनुसूची सिद्धांतहीन फ्लोर क्रॉसिंग या दलबदल की कुप्रथा पर अंकुश लगाकर हमारे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से काम करती है। केंद्र सरकार 52वां संशोधन अधिनियम, 1985 पारित करने और विवादास्पद दसवीं अनुसूची को पेश करने में अपनी वैधानिक शक्तियों और कानून की रूपरेखा के भीतर है।
दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के संबंध में न्यायालय ने सबसे पहले संसदीय लोकतंत्र की जटिल प्रणाली का विश्लेषण किया और निष्कर्ष पर पहुंचा। प्रकाश सिंह बादल बनाम भारत संघ (1987) के मामले को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र जटिल है और साथ ही लोकतंत्र की एक प्रभावी प्रणाली भी है। निर्वाचन क्षेत्र, चुनावी दलों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच संबंधों के कई पहलू और निहितार्थ हैं। कभी-कभी चुनावी दल के विश्वास और मूल्य निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और उनकी मांगों के साथ टकराव में आ सकते हैं।
ऐसे में उस पार्टी का चुना हुआ प्रतिनिधि दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका अपनी पार्टी के प्रति दायित्व होता है, तो दूसरी तरफ उसका उन लोगों के प्रति कर्तव्य होता है जिन्होंने उन्हें चुना है और उन्हें उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए उनकी ओर से काम करने का अधिकार दिया है। क्षमता और निष्ठा का द्वंद्व ही दुविधा पैदा करता है। यहां मौलिक सिद्धांत या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार काम आता है। इस सिद्धांत के अनुसार, निर्वाचित सदस्य पार्टी के लिए वोट कर सकता है अगर उसे लगता है कि यह उसका दायित्व है और बिल या अन्य संसदीय कार्यवाही में पार्टी की दिशा और उद्देश्य उसके मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर, निर्वाचित सदस्य को पार्टी के खिलाफ वोट करने की भी स्वतंत्रता है अगर उसे लगता है कि बिल पारित करने में पार्टी का उद्देश्य उन मतदाताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा नहीं करता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार की क्रॉस-वोटिंग के कई उदाहरण सामने आए हैं और संसदीय लोकतंत्र में यह एक ऐसी विशेषता है जिसे संजोकर रखने की आवश्यकता है।
इसके बाद न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 की भाषा पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि यह निर्वाचित सदस्य की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या पसंद और असहमति की व्यापक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। पैराग्राफ 2, उप-पैराग्राफ 1, खंड b में ऐसे सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान है जो राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए “किसी निर्देश” के विपरीत मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है। हालांकि, यह प्रावधान दो अपवादों को मान्यता देता है: जब वह उस राजनीतिक दल से अनुमति प्राप्त करता है जिससे वह संबंधित है कि वह मतदान के खिलाफ मतदान करे या मतदान से दूर रहे, और जब राजनीतिक दल द्वारा ऐसे मतदान से दूर रहने या क्रॉस-वोटिंग के लिए उसकी निंदा की जाती है। याचिकाकर्ताओं के आरोप का जवाब इन अपवादों में मिलता है। यह प्रावधान ऐसे उदाहरणों की संभावना को मान्यता देता है जब कोई सदस्य उस दल, जिससे वह संबंधित है के खिलाफ मतदान कर सकता है या मतदान नहीं भी कर सकता है। न्यायालय ने माना कि यह प्रावधान अपने आप में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के प्रश्न को हल करता है क्योंकि यह निर्वाचित सदस्यों को विधायिका के सदस्यों के रूप में अपने स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक गुंजाइश देता है।
न्यायालय ने इस तथ्य को दोहराया कि संसदीय लोकतंत्र में, किसी सदस्य द्वारा कार्यपालिका को उसकी शक्ति में बनाए रखना या विपक्ष पर काबू पाने में उसकी मदद करना स्वाभाविक रूप से विरोधाभासी नहीं है, साथ ही कार्यपालिका के काम की जांच करना ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके और यह देखा जा सके कि शक्ति का उचित और वैध तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए, न्यायालय ने फैसला किया कि दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार या लोकतंत्र में पसंद या असहमति के अधिकार के व्यापक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है।

याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर विचार करते हुए न्यायालय ने इस तथ्य को चुनौती दी कि जब कोई व्यक्ति दलबदल करता है या अपना राजनीतिक संगठन बदलता है, तो यह बुराई का मामला बनता है और उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन जब किसी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा या किसी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों का समूह अपना राजनीतिक दल बदलता है, तो वह सामूहिक अपराध दलबदल नहीं माना जाता है। न्यायालय ने यहाँ “दलबदल” और “विभाजन” की अवधारणाओं के बीच अंतर पर जोर दिया। जब कोई व्यक्ति बुराई या नापाक कारणों से अपना दल बदलता है, तो यह दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर, विभाजन तब होता है जब एक पार्टी का एक बड़ा हिस्सा मूल पार्टी से अलग हो जाता है और एक नई पार्टी बनाता है।
इसके अलावा, न्यायालय ने विलय की अवधारणा पर भी जोर दिया। विभाजन और विलय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब विलय होता है, तो एक पार्टी का एक बड़ा हिस्सा मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। यहाँ, न्यायालय ने माना कि जब विभाजन या विलय होता है, तो यह एक राजनीतिक दल के एक बड़े हिस्से की सामूहिक अंतरात्मा होती है कि वे मूल पार्टी से जुड़े नहीं रहना चाहते क्योंकि पार्टी के सदस्यों के एक बड़े हिस्से की सोच में सामूहिक परिवर्तन या बदलाव हुआ है। यह पार्टी के सदस्यों के एक बड़े हिस्से की सामूहिक अंतरात्मा होती है, जहाँ वे सोचते हैं कि वे न केवल मूल पार्टी से अलग होना चाहते हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। पसंद की यह स्वतंत्रता और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संसदीय लोकतंत्र में अंतर्निहित है और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अनुच्छेद 2 दलबदल और विभाजन/विलय के बीच एक रेखा खींचता है। यह एक अपवाद प्रदान करता है, अर्थात, जब किसी पार्टी के एक तिहाई सदस्य अपना राजनीतिक संगठन बदलते हैं या किसी अन्य पार्टी में विलय करते हैं, तो यह विवादित अनुसूची के तहत दलबदल के लिए जिम्मेदार नहीं है। न्यायालय ने अनुसूची के अनुच्छेद 2 को संवैधानिक रूप से वैध मानते हुए कहा कि निर्वाचित सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने की बुरी प्रथा पर अंकुश लगाते हुए, विधायिका ने अनुच्छेद 2 के अपवाद के साथ, ईमानदार असहमति के आधार पर इस तरह के दलबदल के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता पर विचार किया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क कि प्रावधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, किसी भी योग्यता से रहित है।
याचिकाकर्ता का यह तर्क कि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) में प्रयुक्त शब्द “अंतिम” अध्यक्ष के निर्णय को अंतिमता प्रदान करता है, अतार्किक और अविवेकपूर्ण है। न्यायालय ने संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुरूप इस खंड की व्याख्या की। इसने माना कि अनुच्छेद 192 के संबंध में, जो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल के निर्णय को अंतिमता प्रदान करता है, ब्रुन्दाबन नायक बनाम भारत चुनाव आयोग एवं अन्य (1965) के मामले में, इस मामले की जांच संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के तहत एक अपील पर इस न्यायालय द्वारा की गई थी, जब रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि निर्णय बाध्यकारी है।
इसी प्रकार, भारत संघ बनाम ज्योति प्रकाश मित्तर (1971) साथ ही भारत संघ एवं अन्य बनाम तुलसीराम पटेल एवं अन्य (1985) में, अनुच्छेद 217(3) (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के निर्धारण के संबंध में राष्ट्रपति के निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति याचिका के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश की शुद्धता और वैधानिकता के मामले की सुनवाई की और उसकी जांच की।
इसलिए न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 6 में अंतिमता खंड केवल यह मानता है कि न्यायिक समीक्षा वर्जित नहीं है, बल्कि यह केवल तभी उपलब्ध है जब सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष का अंतिम निर्णय आ चुका हो। अनुच्छेद 6 में जिस निष्ठा की बात की जा रही है, वह इस तथ्य का संकेत है कि संसद और राज्य विधानसभाओं का एक पूर्ण आंतरिक मामला होने के नाते, अध्यक्ष, जो न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, के पास इस मामले से निपटने की पहली शक्ति है। पहली बार में संसदीय मुद्दा होने के कारण, यह अयोग्यता के मामलों से निपटने के लिए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को रोकता है, और उनकी शक्ति अध्यक्ष के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही लागू होती है।
फिर भी न्यायालय ने माना कि जहां तक अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा का सवाल है, न्यायालयों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध है, लेकिन यह पूरी तरह से न्यायोचित है। संसदीय और विधानसभा कार्यवाही का न्यायिक प्राधिकारी अध्यक्ष होता है। इसलिए, यदि दसवीं अनुसूची और उसके विवादित प्रावधान विधायी कार्यवाही में न्यायालयों के भारी हस्तक्षेप से अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हैं, तो यह कानून के दायरे में है। फिर भी, न्यायालय के पास मनमानी, दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही और संबंधित अयोग्यता कार्यवाही में अध्यक्ष के आदेश में प्राकृतिक न्याय के नियमों को नकारने वाली घोर त्रुटि के मामलों में न्यायिक समीक्षा का अधिकार है।
असहमतिपूर्ण निर्णय
अल्पमत असहमति वाला निर्णय माननीय न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा और न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा ने सुनाया था। इन न्यायाधीशों की राय न्यायालय के बहुमत के निर्णय से भिन्न थी। उन्होंने कहा कि दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 7, स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों में, सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है और न्यायिक समीक्षा पर सीधा प्रहार करता है जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। प्रमुख रूप से, यह अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों को अध्यक्ष के निर्णय के संबंध में न्यायिक जांच की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की शक्ति को बाहर करता है, इस तथ्य के बावजूद कि लोकतंत्र में, मुख्य न्यायाधिकरण देश की न्यायपालिका होनी चाहिए।
पैराग्राफ 6 में आते हुए, न्यायाधीशों ने माना कि अध्यक्ष को दलबदल और उसके बाद अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार प्रदान करके, यह अदालतों के किसी भी हस्तक्षेप को पूरी तरह से रोकता है और ऐसे अयोग्य सदस्य को न्याय पाने के लिए अदालतों में जाने से रोकता है, जो भारतीय संविधान में निहित न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन है। असहमति जताने वाले न्यायाधीशों की राय में, यह एक बुरा कानून था और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा, इस सवाल पर कि क्या अनुसमर्थन की आवश्यकता है या नहीं, असहमति जताने वाले न्यायाधीशों की राय थी कि चूंकि नई अनुसूची और संशोधन अनुच्छेद 136, 226 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों और अधिकार को काफी हद तक बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 2 के तहत परिकल्पित योजना का पालन करना चाहिए। विस्तार से बताने के लिए, उनका मत था कि दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 7 अनुच्छेद 136, 226 और 227 की योजना को बदलता है और भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को दी गई न्यायिक शक्तियों को छीन लेता है। इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत निर्धारित कुल राज्यों की कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। इसके आधार पर, यह माना गया कि चूंकि संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करने से पहले, उक्त मामले में कोई अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिए संपूर्ण दसवीं अनुसूची ने संवैधानिक योजना का उल्लंघन किया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
पृथक्करण के सिद्धांत के संबंध में, अल्पमत की राय में कहा गया कि यह सिद्धांत तब लागू होता है जब किसी विशेष कानून का कोई विशिष्ट भाग संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, और जैसा कि विवादित मामले में देखा गया है, दसवीं अनुसूची पूरी तरह से अनुच्छेद 136, 226 और 227 के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। जहां तक वर्तमान परिदृश्य का सवाल है, उक्त सिद्धांत का कोई भी अनुप्रयोग नहीं है। इसलिए, यह माना गया कि न केवल पैराग्राफ 7 को खत्म किया जाना चाहिए, बल्कि भारतीय संविधान के मूल मानदंडों का अनुपालन न करने के आधार पर पूरी अनुसूची को भी पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए।
भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक ढांचे का उल्लेख करते हुए, अल्पमत के निर्णय में यह राय थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी संरचना बनाते हैं। भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में, राज्य विधानसभाएं और संसद, देश के लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य अपने मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। इसलिए, वह उनके अधिकारों और हितों को पूरा करने के लिए बाध्य है। कई बार, उनके अधिकार और हित उस पार्टी के रुख से मेल नहीं खाते हैं जिससे सदस्य संबंधित है। ऐसी स्थिति में, सदस्य अपने मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए मतदान करने या मतदान से दूर रहने के लिए लोकतांत्रिक दायित्व के तहत है, और इस प्रकार वह उस राजनीतिक दल के रुख से विचलित होता है जिससे वह संबद्ध है। यह लोकतंत्र में काफी बुनियादी है और असहमति और पसंद के अधिकार की एक विशेषता है, जैसा कि भारतीय संविधान के सार में परिकल्पित है। अतः दसवीं अनुसूची में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी पार्टी के रुख के विपरीत मतदान करने से पहले उस पार्टी की अनुमति लेनी होगी, जो मूल ढांचे और असहमति के महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार में बाधा डालती है, तथा यह असंवैधानिक है।
याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की दलील पर आते हुए, अल्पमत की राय याचिकाकर्ताओं की राय से सहमत थी। यह माना गया कि जहां तक विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता कार्यवाही का सवाल है, अध्यक्ष अंतिम मध्यस्थ नहीं हो सकते। दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 में यह निर्धारित किया गया है कि दलबदल के मामले में विधानसभा या संसद के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार अध्यक्ष के पास है, लेकिन यह प्रथम दृष्टया असंवैधानिक है। इसे प्रमाणित करने के लिए, न्यायालय का तर्क याचिकाकर्ता की इस चिंता पर आधारित था कि अध्यक्ष का चुनाव आम तौर पर इस आधार पर किया जाता है कि सदन में किस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत सीटें हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब अध्यक्ष चुना जाता है, तो वह आम तौर पर बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, लोकतांत्रिक राजनीति में अध्यक्ष का पद एक पवित्र स्थान रखता है, लेकिन यह मान लेना कि वह हर समय निष्पक्ष रहेगा, व्यावहारिक रूप से असंभव है क्योंकि वह किसी राजनीतिक दल या गठबंधन से जुड़ा हुआ है। इसलिए, अध्यक्ष को स्वतंत्र निर्णायक प्राधिकारी नहीं माना जा सकता और उसे अयोग्यता का फैसला करने के लिए अंतिम प्राधिकारी बनाना स्पष्ट रूप से मनमाना है। इसलिए, दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 भारतीय संविधान की योजना का खंडन करता है।
अंत में, न्यायालय की अल्पमत राय ने माना कि अध्यक्ष के सभी निर्णयों को अंतिमता प्रदान करने वाले अनुच्छेद 102 और 191 की योजना में परिवर्तन को निरस्त किया जाना चाहिए।

किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्लु (1993) का विश्लेषण
यह मामला भारतीय लोकतंत्र में दलबदल विरोधी कानून के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में कार्य करता है। इसने 52वें संशोधन अधिनियम, 1958 और इसलिए दसवीं अनुसूची की वैधता पर जोर देकर दलबदल विरोधी कानून की संवैधानिक वैधता स्थापित की। यह मामला विधायी व्याख्या के नियम के लिए एक मिसाल के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि यह इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराता है कि किसी कानून और उसके प्रावधानों की व्याख्या पूरी तरह से की जानी चाहिए, न कि अलग-अलग। निर्माण के इस सिद्धांत का उपयोग करके ही न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज कर दिया और कानून की वैधता पर जोर दिया। यह निर्णायक फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला और भारतीय लोकतंत्र के दोनों अंगों द्वारा हस्तक्षेप की सीमाओं के संबंध में गंभीर अस्पष्टताओं को दूर किया। इसने इस नियम को फिर से स्थापित किया कि देश की विधायिका के प्रभावी कामकाज के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है, लेकिन न्यायपालिका की अपनी सीमाएँ हैं और वह न्याय देने की आड़ में कानून बनाने के कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती।
दलबदल विरोधी कानून की आवश्यकता
दलबदल विरोधी कानून के कई उद्देश्य हैं। मुख्य रूप से, इस कानून की आवश्यकता भौतिक लाभों के लालच और अन्य नापाक उद्देश्यों से प्रेरित दलबदल को रोकने के लिए है, जिसमें रिश्वत, विभिन्न प्रकार के उपकार आदि शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की भावना को बाधित करते हैं। इसलिए, यह भारत के लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद करता है।
दलबदल विरोधी कानून के लाभ
दलबदल विरोधी कानून विधायकों को किसी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने राजनीतिक संघ को बदलने से रोकता है। इसके अलावा, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक स्थिर सरकार की आवश्यकता होती है और दलबदल विरोधी कानून, राजनीतिक संबद्धता के अवैध और अनुचित परिवर्तन को प्रतिबंधित करके, ऐसी स्थिरता को बनाए रखता है। यह कानून एक स्वस्थ लोकतांत्रिक ढांचे के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है।
इसके अलावा, कभी-कभी विपक्षी दल सत्ता पक्ष के सदस्यों को रिश्वत देकर किसी राज्य या देश की सरकार को गिराने की कोशिश करता है और अगर यह काम करता है, तो सरकार में अचानक बदलाव हो सकता है या सरकार गिर सकती है। दलबदल विरोधी कानून इसे रोकता है। इसके अलावा, यह सदस्यों की अयोग्यता के बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक विलय की अनुमति देता है, जिससे चुनने और असहमति के अधिकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। बड़े पैमाने पर, यह लोकतंत्र की संस्था को मजबूत करता है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है।
दलबदल विरोधी कानून के नुकसान
दलबदल विरोधी कानून के सबसे अधिक आलोचनात्मक पहलुओं में से एक यह है कि यह विधायिका के सदस्य के उस अधिकार का अतिक्रमण करता है, जिसके तहत वह अपने मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए पार्टी के रुख के विपरीत चुनाव कर सकता है।
दलबदलुओं को दंडित करने और उन्हें इस आधार पर अयोग्य ठहराने के अधीन करके कि उन्होंने पार्टी से पूर्व अनुमोदन और अनुमति के बिना पार्टी के विरोध में मतदान किया है, दलबदल विरोधी कानून अंतर-पार्टी लोकतंत्र की अवधारणा का उल्लंघन करता है। लोकतंत्र एक सर्वव्यापी अवधारणा है और ऐसा कोई विशेष प्रावधान या कोड नहीं है जो कहता है कि किसी पार्टी के भीतर असहमति का कोई अधिकार नहीं है और पार्टी के सभी सदस्य पार्टी के निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। आजादी के बाद से ऐसे उदाहरण हैं, जिनमें एक पार्टी के सदस्य ने पार्टी की राय से परे काम किया है, जो लोकतंत्र में असहमति की मूल विशेषता है। हालांकि, दूसरी ओर, दसवीं अनुसूची में प्रदान की गई दलबदल विरोधी योजना, विरोध में मतदान करने या परहेज करने से पहले पार्टी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाकर, अंतर-पार्टी लोकतंत्र की अवधारणा का स्पष्ट उल्लंघन है।
यह आरोप लगाया गया है कि अयोग्य ठहराए जाने की धमकी का उपयोग करके, एक राजनीतिक दल का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के असहमत सदस्यों को पार्टी के नेतृत्व के निर्देशों के विरुद्ध न जाने के लिए मजबूर कर सकता है और यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे अयोग्य ठहराए जाने के अधीन होंगे। यह किसी सदस्य के लिए अपनी पार्टी के अनुरूप मतदान करना अनिवार्य बनाता है, भले ही वह जानता हो कि पार्टी उस मतदाता वर्ग के अधिकारों और हितों के विपरीत है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना को बाधित करता है। प्रत्येक राजनीतिक प्रतिनिधि अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और पहली जिम्मेदारी उनके हितों को पूरा करना है न कि उस राजनीतिक दल के हितों को जिससे वह संबंधित है।

निष्कर्ष
भारत जैसे लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज के लिए दलबदल विरोधी कानून जरूरी है। यह अवैध रूप से पार्टी बदलने की घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हुआ है। इस मामले में कानून की वैधता पर जोर देकर अदालत ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कानून को सील कर दिया है। निष्कर्ष के तौर पर, यह कानून कई परिस्थितियों में कारगर साबित हुआ है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इसे लाया गया था, उसे पूरा करने में विफल रहा है। दलबदल विरोधी कानून में अभी भी छोटी-छोटी खामियां हैं और राजनेता इन खामियों का फायदा उठाकर निषेधात्मक कानून की जांच से बच निकलते हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखना और कानून को मजबूत बनाना भारत की विधायिका और न्यायपालिका पर निर्भर करता है ताकि इसकी प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
इस मामले में कौन सा कानून प्रासंगिक है?
यह मामला दलबदल विरोधी कानून से संबंधित है।
52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई?
52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
दसवीं अनुसूची के किस अनुच्छेद को न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया?
न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 7 को असंवैधानिक घोषित किया।
संदर्भ







