यह लेख Shilpi द्वारा लिखा गया है। इस लेख में हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1954) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णय का विस्तृत विश्लेषण है। यह आवश्यक विधायी कार्यों की अवधारणा और विधायिका द्वारा कार्यपालिका को उनके प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
जब हम ‘अत्यधिक प्रत्यायोजन’ शब्द के वर्णनात्मक अर्थ पर गौर करते हैं, तो हम नाम से ही इसका अर्थ समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति स्वयं-व्याख्यात्मक है – एक प्राधिकरण अपने कार्यों या अपने अधिकार के हिस्से को कानूनी रूप से अनुमत सीमा से अधिक किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपता है।
इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने पर हम देख सकते हैं कि सरकार का विधायी निकाय कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है जबकि सरकार का कार्यकारी निकाय विधानमंडल द्वारा अपनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इस परिदृश्य में अत्यधिक प्रत्यायोजन के तहत, विधानमंडल अपने कार्य, यानी कानून बनाने की शक्तियों को कार्यपालिका को सौंपता है जो बाद में इसे अपने अधीन निचले प्राधिकारी को सौंपती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, अन्य देशों के विपरीत, भारत एक ही भाषा, संस्कृति, लोगों या धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जबकि कोई भी अन्य देश इन मतभेदों को विवाद का कारण और चिंताओं से भरा मानता, भारत अपनी विविधता में एकता खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सामने आया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और 15 अगस्त 1947 का दिन भारत की स्वतंत्रता-पूर्व कार्यपालिका की प्रधानता से लेकर स्वतंत्रता के निकट और उसके बाद कार्यपालिका की प्रधानता तक की यात्रा का चरम बिन्दु रहा है।
संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए बनाया था, लेकिन इसमें एकात्मक तत्व शामिल हैं। यह दोहरी राजनीति इसलिए संभव हुई क्योंकि केंद्र ने राज्यों को उचित स्वायत्तता (ऑटोनोमी) दी और बदले में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संघ बनाने के लिए एकीकरण नहीं किया। सरल शब्दों में, भारत का यह स्वरूप स्वतंत्रता से पहले अस्तित्व में था। राज्य, प्रांत (प्रेसिडेंसियाँ) और राज्य एक दूसरे में विलीन हो गए और कुछ ने अपना नाम बदल लिया। आज, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
भारत का लोकतंत्र अपने नाम के अनुरूप चार स्तंभों पर निर्भर करता है – विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। जबकि इन चार स्तंभों के कार्य विशिष्ट हैं, वे देश में लोकतंत्र की सच्ची भावना को सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे पर नज़र रखने में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। वे सभी भारत को हिंसा, नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी), भ्रष्टाचार, अराजकता आदि की घटनाओं से बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
भारतीय लोकतंत्र के अर्ध-संघीय ढांचे पर विचार करते हुए, इस लेख का उद्देश्य ऐसे ही एक ऐतिहासिक मामले पर चर्चा करना है, जहां न्यायालय ने आवश्यक विधायी कार्यों की रूपरेखा और शक्तियों के पृथक्करण (सेपरेशन) के सिद्धांत को परिभाषित किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार में कोई भी व्यक्ति आवश्यक विधायी कार्यों के अत्यधिक हस्तांतरण में भाग नहीं ले सके।

मामले का विवरण
मामले के मूलभूत विवरण निम्नलिखित हैं:
- न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- अपीलकर्ता: हरिशंकर बागला और अन्य
- प्रतिवादी: मध्य प्रदेश राज्य
- मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 7, 1953
- तटस्थ उद्धरण (साइटेशन): (1954) 1 एससीसी 978; एआईआर 1954 एससी 465
- पीठ: एम.सी. महाजन, सी.जे., बी.के. मुखर्जी, विवियन बोस, एन.एच. भगवती और टी.एल. वेंकटराम अय्यर, जे.जे.
- निर्णय की तिथि: 14.05.1954
- प्रासंगिक अधिनियम: आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946; सूती वस्त्र (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1948।
- अधिनियम की प्रासंगिक धारा(एँ): आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946 की धाराएँ 3, 4, 6 और 7; सूती वस्त्र (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 2, 3, 4, 8।
मामले की पृष्ठभूमि
हरिशंकर बागला एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1954) मामले का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा 14.05.1954 को किया गया। यह मामला मुख्य रूप से आवश्यक विधायी कार्यों की अवधारणा और उसके प्रत्यायोजन की सीमा से संबंधित है। यह मामला सूती वस्त्र (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1948 (जिसे आगे “आक्षेपित आदेश” कहा जाएगा) की वैधता से संबंधित प्रश्न से संबंधित था, जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा कपड़े के परिवहन के लिए वस्त्र आयुक्त से अनुज्ञा पत्र (परमिट) लेने का प्रावधान था। पक्ष ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश अनुज्ञा पत्र देने या न देने के लिए अनियमित और मनमाने अधिकार प्रदान करता है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश की वैधता को बरकरार रखा।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रत्यायोजित विधान जो मूल अधिनियम के अन्तर्गत आता है, उसे अन्य विधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधिकारातीत (अल्ट्रा वायरस) माना जा सकता है। हालाँकि, किसी कानून में ऐसा प्रावधान हो सकता है जो उस कानून के अन्तर्गत बनाए गए नियमों को किसी अन्य कानून के साथ असंगति के आधार पर अमान्य होने से बचा सकता है। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में बरकरार रखा।
हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1954) के तथ्य
अपीलकर्ता और उसकी पत्नी को आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जाएगा) की धारा 7 के प्रावधानों के साथ आक्षेपित आदेश के खंड (3) का उल्लंघन करने के लिए रेलवे पुलिस बल द्वारा 29.11.1948 को इटारसी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। अपीलकर्ता के पास 6 मन से ज़्यादा वज़न का “नया सूती कपड़ा” पाया गया। आरोप लगाया गया कि पक्ष ने बिना किसी ज़रूरी अनुज्ञा पत्र के बॉम्बे से कानपुर तक “नया सूती कपड़ा” ले गया। पारित चालान को उच्च न्यायालय ने वापस ले लिया क्योंकि इसमें संवैधानिक मुद्दों पर निर्णय शामिल था।
उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.09.1952 के आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों को बरकरार रखा। अधिनियम की धारा 6 को रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के साथ असंगत माना गया। हालांकि, न्यायालय ने निर्णय किया कि धारा 6 की असंवैधानिकता वर्तमान मामले में अभियोजन को प्रभावित नहीं करेगी। उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन को आगे बढ़ाने और कानून के प्रावधानों के अनुसार मामले की सुनवाई करने के लिए रिकॉर्ड को निचली अदालत में वापस करने के निर्देश दिए गए।
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को अपील करने की अनुमति दी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 और 134 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद वर्तमान अपील दायर की गई।
मामले के प्रासंगिक प्रावधान और सिद्धांत
आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 3
अधिनियम की धारा 3 आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियों से संबंधित है।
- जब केन्द्रीय सरकार को लगता है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना आवश्यक या लाभदायक है, या यह सुनिश्चित करना है कि आपूर्ति कुछ चयनित लोगों के बजाय सभी वर्गों में समान रूप से वितरित की जाए और उचित मूल्य पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो, तो केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण, आपूर्ति या वितरण और साथ ही इसके व्यापार और वाणिज्य (कमर्शियल) के विनियमन और निषेध के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है।
- जबकि केंद्र सरकार के पास इस प्रावधान की उप-धारा (1) के अनुसार सामान्य शक्तियां हैं, सरकार निम्नलिखित के संबंध में आदेश जारी कर सकती है –
- अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस या किसी अन्य माध्यम से किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण को विनियमित करना।
- अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस या किसी अन्य माध्यम से किसी भी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग या उपभोग को विनियमित करना।
आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946 की धारा 4
अधिनियम की धारा 4 केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है। केंद्र सरकार को यह अधिसूचित करने और निर्देश देने की शक्ति है कि ऐसे मामलों और ऐसी शर्तों से संबंधित धारा 3 के तहत उसके द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित द्वारा भी किया जा सकता है –
- कोई अधिकारी या कोई प्राधिकरण जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, या
- ऐसी राज्य सरकार या कोई अधिकारी या प्राधिकरण जो राज्य सरकार के अधीनस्थ है, जैसा कि निर्देश में वर्णित या उल्लेख किया गया है।
आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946 की धारा 6
अधिनियम की धारा 6 उन परिस्थितियों के बारे में बताती है जिनके तहत धारा 3 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अन्य मौजूद अधिनियमों के साथ असंगत हैं।
धारा 6 यह घोषित करती है कि यदि धारा 3 के अनुसार बनाए गए आदेश और किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई असंगति है, तो उस असंगति के बावजूद, आदेश के प्रावधान अन्य अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होंगे।
सूती वस्त्र (संचालन नियंत्रण) आदेश, 1948 का खंड 2
आक्षेपित आदेश का खंड 2 निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करता है:
- परिधान (अपैरल) – कोई भी परिधान या अन्य वस्तु जो पूरी तरह से या मुख्य रूप से ऐसे कपड़े से बनी हो जो बुना हुआ कपड़ा न हो और जिसका उपयोग घरेलू या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाता हो। इसमें पुराने या इस्तेमाल किए गए कपड़ों का उपयोग शामिल नहीं है।
- वाहक – जब रेलवे प्रशासन या कोई अन्य व्यक्ति हवाई, समुद्री, भूमि या अंतर्देशीय नौवहन के माध्यम से संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के व्यवसाय में लगा हो।
- होजरी – इसका अर्थ है मोजे, बनियान, दराज या व्यक्तिगत उपयोग की कोई अन्य वस्तु जो बुने हुए कपड़े से बनाई गई हो या सीधे धागे से बुनी गई हो।
- इसमें कहा गया है कि कपड़ा और धागे का अर्थ वही है जो सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 में दिया गया है।
- वस्त्र आयुक्त – जब केंद्र सरकार किसी को वस्त्र आयुक्त के पद पर नियुक्त करती है, तो उक्त व्यक्ति को इस आदेश के नियमों के अनुसार वस्त्र आयुक्त माना जाएगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त, उप वस्त्र आयुक्त और अन्य भी शामिल हैं।
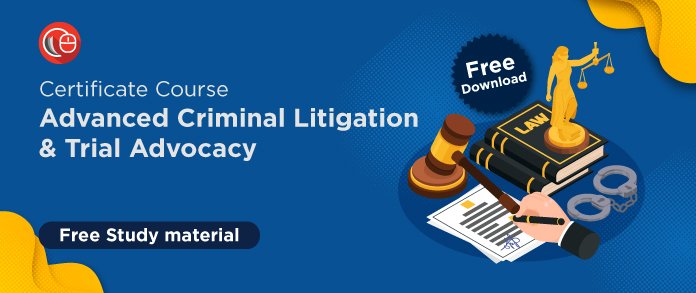
सूती कपड़ा (संचलन पर नियंत्रण) आदेश, 1948 का खंड 3
आक्षेपित आदेश के खंड 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए बिना भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवाई, रेल, सड़क, समुद्र या अंतर्देशीय नौवहन द्वारा किसी कपड़े, धागे या परिधान का परिवहन नहीं कर सकता है या परिवहन में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है:
- वस्त्र आयुक्त को ग्रेटर बॉम्बे और अहमदाबाद शहर के क्षेत्रों के अलावा किसी विशेष राज्य में एक स्थान से उक्त वस्तुओं के परिवहन के लिए उस राज्य की सरकार द्वारा सामान्य अनुज्ञा पत्र के बारे में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी होगी।
- वस्त्र आयुक्त को विशेष परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना होगा।
सूती कपड़ा (संचलन पर नियंत्रण) आदेश, 1948 का खंड 8
आक्षेपित आदेश के खंड 8 में कहा गया है कि कपड़ा आयुक्त को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, जिसमें यह बताया जा सके कि इस आक्षेपित आदेश के तहत विशेष अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति किस तरह से ऐसा कर सकता है। अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेदन के विभिन्न प्रपत्रों और जिन परिस्थितियों में अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
आवश्यक विधायी कार्य
कानून बनाने की शक्ति अनिवार्य रूप से विधानमंडल को दी गई है, हालांकि, कुछ परिस्थितियों में इन विधायी कार्यों को कुछ शर्तों के अधीन सौंपने की अनुमति है। फिर भी, विधानमंडल अपने आवश्यक विधायी कार्यों को सौंप नहीं सकता है। आवश्यक विधायी कार्य की किसी भी पूर्ण परिभाषा के अभाव में, शून्य को भरने के लिए, न्यायपालिका ने विभिन्न अधिनियमों की व्याख्या की है जो आवश्यक विधायी कार्य के दायरे में आएंगे।
दिल्ली कानून अधिनियम, 1932, अजमेर-मेरवाड़ा (विस्तार) बनाम भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 (1951) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आवश्यक विधायी कार्य में विधायी नीति का निर्धारण या चयन शामिल है। इसमें नीति को औपचारिक रूप से लागू करके उसे आचरण का बाध्यकारी नियम बनाना भी शामिल है। नीति के विवरण के दायरे को तैयार करने का विवेकाधिकार विधानमंडल के पास है और शेष विधायी कार्य अधीनस्थ प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है ताकि वह नीति के दायरे में रहते हुए विवरण तैयार कर सके।
हमदर्द दवाखाना (वक्फ) लाल कुआं, दिल्ली और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1959) के मामले में, जहां औषधि और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 को लाइलाज बीमारियों के इलाज का दावा करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था, और अधिनियम की धारा 3 ने सरकार को बीमारियों के नामों वाली सूची को संशोधित करने का अधिकार प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को असंवैधानिक माना क्योंकि यह धारा इसके लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश प्रदान करने में विफल रही।
देवी दास गोपाल कृष्णन एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (1967) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी राज्य की विविध गतिविधियों को देखते हुए, राज्य विवादों के विभिन्न पहलुओं के अनुसार सभी जटिलताओं को हल नहीं कर सकता। इसलिए, विवरणों को हल करने का कार्य कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकरण को सौंपना आवश्यक है।
दिल्ली नगर निगम बनाम बिरला कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स दिल्ली (1968) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधानमंडल को आवश्यक विधायी कार्यों को सौंपने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा विधानमंडल को विशेष रूप से सौंपे गए विषय के संबंध में विधायी कार्य या अधिकार का पूरी तरह या आंशिक रूप से त्याग नहीं किया जा सकता है।
गैमन इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य (1974) के मामले में, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 34 ने किसी भी कठिनाई के मामले में अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 34 अत्यधिक प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं करती है, क्योंकि यह अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन नहीं करती है, बल्कि यह अधिनियम को उचित रूप से क्रियान्वित करने के तरीके प्रदान करती है।
विधानमंडल का आवश्यक विधायी कार्य क्या है, यह तय करना न्यायालय की जिम्मेदारी है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वह जांच करे कि विवादित प्रत्यायोजित विधान मूल विधान के दायरे में आता है या नहीं। प्रतिनिधि को ऐसे संशोधन करने का अधिकार नहीं है, जो मूल विधान की अंतर्निहित नीति को बदलने की क्षमता रखते हों। प्रतिनिधि के लिए संशोधन करते समय मूल विधान के सार और तत्व को ध्यान में रखना अनिवार्य है।
प्रत्यायोजन का सिद्धांत
प्रत्यायोजन का सिद्धांत उस अधिनियम को संदर्भित करता है, जिसमें संसद के अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को अपनी ओर से कानून बनाने की अनुमति दे सकता है। प्रत्यायोजित विधान के सिद्धांत को ‘द्वितीयक विधान’ के रूप में भी जाना जाता है।
संसद किसी भी कानून का ढांचा तैयार करती है और अधिनियम के उद्देश्य के लिए कानून की रूपरेखा निर्धारित करती है। फिर, संसद कानून बनाने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को सौंपती है ताकि वह अधिनियम के कानूनों को व्यापक तरीके से परिभाषित कर सके। इसलिए, प्राथमिक प्रत्यायोजन का तरीका जो संसद का अधिनियम है, किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से नियम या कानून बनाने की अनुमति देता है। जिस प्राधिकरण को विधान बनाने की शक्तियाँ सौंपी गई हैं, उसके द्वारा बनाए गए कानून अधिनियम के परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार होने चाहिए।
चूंकि प्रत्यायोजन की रूपरेखा को कड़ाई से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए न्यायपालिका ने समय-समय पर उन सीमाओं का पता लगाने के लिए कदम उठाया है जिनके भीतर संसद द्वारा कानून बनाने की यह शक्ति प्रत्यायोजित की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्यायोजन भारतीय संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक प्रत्यायोजन के बराबर न हो। आइए उन पर एक नज़र डालें:
दिल्ली कानून अधिनियम मामले (1951) में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कनिया ने कहा कि भले ही विधानमंडल को अधिनियम के निर्बाध संचालन और उसे प्रभावी बनाने के लिए नियम और विनियमन बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसे इस कार्य को करते समय आचरण के नियम बनाने वाली नीति और सिद्धांतों को निर्धारित करना चाहिए। केवल युद्ध जैसे आपातकाल के मामलों के दौरान ही हमारे देश के विधायी निकाय को किसी गैर-विधायी प्राधिकरण को व्यापक विवेक के साथ नियम बनाने की शक्ति सौंपनी चाहिए।
अजय कुमार बनर्जी बनाम भारत संघ (1984) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विधायी नीति की घोषणा करने तथा नीति के मानकों को अत्यंत सटीकता से परिभाषित करने की भूमिका आवश्यक विधायी कार्य के दायरे में आती है, अतः इसे विधायी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता।
कृषि बाजार समिति बनाम शालीमार केमिकल वर्क्स लिमिटेड (1997) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधायी निकाय द्वारा प्रत्यायोजन का प्रयोग केवल कार्यान्वयन उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अधीनस्थ विधान की भूमिका नीति को कार्यात्मक बनाने तक सीमित है, न कि नीति विकल्पों के बारे में विचार-विमर्श करने या उन्हें शुरू से बनाने तक, क्योंकि यह उन उद्देश्यों के विरुद्ध होगा जिनके लिए विधायी निकाय द्वारा गैर-विधायी निकाय को पहली बार में शक्तियाँ सौंपी गई थीं।
ग्वालियर रेयान सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (डब्ल्यूवीजी) कंपनी बनाम सहायक बिक्री आयुक्त (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधायी नीति तैयार करना आवश्यक विधायी कार्यों का एक अनिवार्य हिस्सा है। आचरण के बाध्यकारी नियम के अनुसार, विधानमंडल के पास इसके निर्माण को सौंपने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा, विधानमंडल के पास अपनी मर्जी और पसंद के अनुसार अधिकार या अपनी शक्तियों को सौंपने का कोई अप्रतिबंधित अधिकार नहीं है। विधानमंडल के लिए यह अनिवार्य है कि वह आवश्यक विधायी कार्यों को केवल अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखे तथा अधीनस्थ विधानों के केवल उन्हीं कार्यों को सौंपे जो किसी अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक हों। मार्गदर्शन किस सीमा तक प्रदान किया गया है तथा क्या किसी मामले में यह प्रदान किया गया है, यह न्यायालय द्वारा संबंधित अधिनियम, उसके उद्देश्य, उसके प्रावधानों तथा उसकी प्रस्तावना पर बारीकी से विचार करने पर निर्भर करता है।
वसंतलाल मगनभाई संजनवाला बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधायी शक्ति समग्र रूप से प्रत्यायोजन की शक्ति से अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में, कार्यपालिका द्वारा विधायिका द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति विधायिका को दी गई विधायी शक्तियों का अभिन्न अंग है। मौजूदा समय ऐसा है कि विधायिका को जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न जटिलताओं को हल करने के लिए अथक प्रयास करना होगा। ऐसे परिदृश्यों में, विधानमंडल को अपने अधिनियमों द्वारा लाई गई विधायी नीति को क्रियान्वित करने के लिए अपनी पसंद की सहायक शक्तियों को सौंपना आसान और महत्वपूर्ण लगता है। किसी भी कीमत पर, विधानमंडल को अपने आवश्यक विधायी कार्यों को सौंपने का अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है। जबकि यह विधायी नीति और सिद्धांत निर्धारित कर सकता है, विधानमंडल का यह कर्तव्य है कि वह प्राधिकरण या किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय को सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करे जिसे वह उक्त नीति के अनुपालन के लिए अपनी सहायक शक्तियाँ सौंप रहा है।
संसद को किसी भी मामले पर कानून बनाने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त नहीं है। भारत के संविधान ने संसद को अपनी ओर से कानून, नियम आदि बनाने की यह शक्ति सौंपी है। इसलिए, संसद मनमाने ढंग से इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। इसके बजाय, संविधान द्वारा संसद को इस शक्ति का प्रयोग स्वयं करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौजूदा कानूनों और संविधान के अनुसार आवश्यक विधायी कार्यों का कोई भी हस्तांतरण सख्त वर्जित है और इन कार्यों को कार्यपालिका को सौंपने के बजाय विधानमंडल द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। हालाँकि, एक बार जब विधानमंडल आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रयोग करने का अपना प्राथमिक कार्य पूरा कर लेता है, तो वह किसी भी या सभी सहायक कार्यों को कार्यपालिका को सौंप सकता है।

उठाए गए मुद्दे
पक्षों के बीच विवाद के निपटारे के लिए, न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर निर्णय लिया गया:
- क्या अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधान और आक्षेपित आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और (g) का उल्लंघन करते हैं?
- क्या अधिनियम की धारा 3 और 4 विधानमंडल द्वारा विधायी शक्तियों के अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर संविधान के विरुद्ध हैं?
- चूँकि अधिनियम की धारा 6 को अधिकारातीत पाया गया है, और धारा 3 धारा 6 के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, क्या धारा 3 को भी अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए?
- क्या आक्षेपित आदेश भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 27, 28 और 41 का उल्लंघन है और इसलिए आक्षेपित आदेश पूर्णतः शून्य है?
पक्षों द्वारा दिए गए तर्क
अपीलकर्ता
अपीलकर्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:
- अधिनियम और आक्षेपित आदेश के प्रावधानों में रेल द्वारा सूती वस्त्रों के परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और (g) में किसी भी पेशे को अपनाने या कोई भी व्यापार करने का अधिकार दिया गया है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता सूती वस्त्रों की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में लगे व्यक्ति के इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
- अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत, वस्त्र आयुक्त को अनुज्ञा पत्र देने या देने से मना करने के लिए अनियमित और मनमाना अधिकार दिया गया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 विधानमण्डल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि बाद वाले द्वारा शक्तियों का अत्यधिक प्रत्यायोजन किया गया है। अधिनियम की धारा 4 पर इस आधार पर आगे हमला किया गया कि केंद्र सरकार को धारा 3 के तहत आदेश देने के लिए किसी अन्य प्राधिकरण को अपनी शक्ति सौंपने का अधिकार है, इसलिए, प्रतिनिधि द्वारा शक्तियों का और अधिक प्रत्यायोजन किया गया है।
- अधिनियम की धारा 6 अन्य अधिनियमों के संबंध में अधिनियम के तहत बनाए गए आदेशों को अधिभावी (ओवररराइडिंग) प्रभाव प्रदान करती है। इस धारा को उच्च न्यायालय ने अमान्य ठहराया था। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम की धारा 6 को अधिकारातीत पाया गया है, इसलिए अधिनियम की धारा 3 को भी अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि अधिनियम की धारा 6 और धारा 3 दोनों ही अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं।
- भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धाराएं 27, 28 और 41 में रेल प्रशासन द्वारा रोलिंग स्टॉक के उपयोग, केन्द्र सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन, तथा एक व्यापारी के लिए कम दर वसूलने के साक्ष्य का भार क्रमशः रेल प्रशासन पर है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश के खंड (3) और (4) वस्त्र आयुक्त को वाहक को बुकिंग या परिवहन बंद करने का निर्देश देने का अधिकार देता है, जो भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 27, 28 और 41 का सीधा उल्लंघन है। आक्षेपित आदेश द्वारा भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 27, 28 और 41 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और इसलिए इसे सभी मामलों में शून्य घोषित किया जाना चाहिए।
प्रतिवादी
प्रतिवादी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:
- प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की, जिसमें कहा गया कि अधिनियम की धारा 6 असंवैधानिक है।
हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1954) में निर्णय
यह तय करते हुए कि क्या अधिनियम की धारा 3 और 4 के प्रावधानों की आवश्यकताएं और आक्षेपित आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और (g) का उल्लंघन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपातकाल की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करना अनिवार्य था। अधिनियम की धारा 2 में आवश्यक वस्तुओं की सूची का उल्लेख किया गया है। इसलिए, ऐसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और (g) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 19(5) में ऐसे प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो सार्वजनिक हित में हैं।
अधिनियम की धारा 3 ने केंद्र सरकार को “किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने, या उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने” के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की। अधिनियम की धारा 6 में प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत बनाए गए नियमों का मौजूदा क़ानूनों पर एक प्रमुख प्रभाव होगा। कानून के प्रचलित सिद्धांतों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 3 और 6 की वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने निर्णय किया कि अधिनियम के तहत अंतर्निहित नीति अधिनियम की धारा 3 के तहत पर्याप्त रूप से तैयार की गई थी, जो प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक समझने योग्य और पर्याप्त उपाय प्रदान करती है।
यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिनिधि को अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्तियों को आगे भी सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 4 में ऐसे व्यक्तियों के वर्ग का प्रावधान है जिन्हें केंद्र सरकार शक्तियों को सौंप सकती है या उन्हें उप-प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि साधनों का चयन विधानमंडल द्वारा स्वयं नहीं किया गया है।
न्यायालय ने माना कि धारा 6 में संशोधन करने की शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रावधान नहीं है। धारा 6 परस्पर विरोधी कानूनों को दरकिनार करने की शक्ति प्रदान करती है। यह निर्णय लिया गया कि यह नियम नहीं थे जिन्होंने मौजूदा क़ानून को दरकिनार किया था, बल्कि यह संसद ही थी जिसने मूल कानून को अन्य मौजूदा क़ानूनों को दरकिनार करने का अधिकार दिया था। इसलिए, भले ही यह माना जाए कि धारा 6 क़ानूनों में संशोधन का प्रावधान करती है, लेकिन यह कार्यपालिका के बजाय विधानमंडल के लिए जिम्मेदार है। न्यायालय ने माना कि धारा 6 के प्रावधानों में कोई प्रत्यायोजन नहीं है और इसलिए, धारा 6 संवैधानिक है।
अगले तर्क पर निर्णय लेते हुए कि आक्षेपित आदेश के प्रावधान रेलवे अधिनियम की धारा 27, 28 और 41 के निहित निरसन के रूप में कार्य करते हैं, न्यायालय ने निर्णय लिया कि आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह दर्शाता हो कि यह रेलवे अधिनियम के प्रावधानों को अधिभावी करता है। आक्षेपित आदेश के खंड केवल रेलवे अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के पूरक हैं और उनका अधिरोहण (सुपरसेड) नहीं करते हैं।
अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धाराएं 3, 4 और 6 संवैधानिक हैं तथा आक्षेपित आदेश भी संवैधानिक और वैध है।
हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1954) में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय
इस मामले में संदर्भित निर्णयों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:
मेसर्स द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य (1954) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के पास आदेश पारित करने की क्षमता है, तथापि उसी आदेश को भारतीय संविधान के भाग III में निहित परीक्षण से गुजरना होगा। यदि उक्त आदेश परीक्षण में खरा नहीं उतरता है, तो न्यायालय के पास उसे रद्द करने का अधिकार है। यदि कोई विधायी आदेश किसी कार्यकारी प्राधिकरण को किसी व्यापार या व्यवसाय की निगरानी करने का अधिकार देता है, तो यह अधिकार अनियंत्रित या मनमाना नहीं होना चाहिए क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत गारंटीकृत नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल लाइसेंस प्रदान और जारी नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ भरे हुए हैं। जबकि विधानमंडल को यह शक्ति किसी कार्यकारी प्राधिकरण को सौंपनी होती है, बाद वाले को दिए गए विवेक को संबंधित आदेश द्वारा प्रदान की गई किसी प्रक्रिया के विरुद्ध परखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवेक का दुरुपयोग न हो। यदि ऐसा कोई परीक्षण या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती है और कार्यकारी प्राधिकरण को इस मामले में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो उसके कार्यों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या दुश्मनी के तत्व शामिल हो सकते हैं जो अनुच्छेद 14 पर अतिक्रमण करेंगे जो बाद में एक भारतीय नागरिक के रूप में किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने की उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा।
अंततः, न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि आक्षेपित आदेश के खंड 3(1) ने राज्य नियंत्रक को अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान की है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) दोनों का उल्लंघन है।
इसके अलावा, आक्षेपित आदेश के खंड 4(3) ने कार्यकारी प्राधिकरण को कोयला बेचने के लिए लाइसेंस देने या रद्द करने की बेलगाम और अनियंत्रित शक्ति दी। इसे भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19(1)(g) दोनों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया। चूंकि इन दो खंडों को आदेश के बाकी हिस्सों को कार्यात्मक बनाने के लिए अलग नहीं किया जा सकता था, इसलिए पूरे आदेश को शून्य माना गया।
पनामा रिफाइनिंग कंपनी बनाम रयान (1935) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आदेश पारित करते समय, राष्ट्रपति ने विधानमंडल की शक्ति का गठन किया था जिसे कांग्रेस को पहले स्थान पर सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए सरकार की किसी अन्य शाखा को विधायी प्रकृति की शक्तियाँ कभी नहीं सौंप सकती।
जॉर्ज वॉकम शैनन एवं अन्य बनाम लोअर मेनलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स बोर्ड एवं अन्य (1938) में मामला संबंधित अधिनियम की वैधता के इर्द-गिर्द घूमता रहा, जिसने विधायी शक्ति के उप-प्रत्यायोजन की भी अनुमति दी। विधान मंडल द्वारा ऐसी शक्ति को लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल को सौंपे जाने के खिलाफ आपत्ति उठाई गई, जिन्होंने इसे आगे विपणन (मार्केटिंग) बोर्ड को सौंप दिया। प्रिवी काउंसिल के लिए निर्णय देते हुए, लॉर्ड एटकिंस ने कहा कि प्रांतीय विधानमंडल द्वारा उप-प्रतिनिधिमंडल के प्रत्यायोजन के प्रति ऐसी आपत्ति विध्वंसकारी थी, जिसका अर्थ है कि बाद वाले द्वारा प्राप्त अधिकारों का हनन। इसलिए, प्रिवी काउंसिल ने अधिनियम को बरकरार रखा।

दिल्ली कानून अधिनियम मामले (1951) में बहुमत के फैसले में कहा गया कि विधानमंडल को अपनी आवश्यक शक्तियों को सौंपने का अधिकार नहीं है। कार्यकारी प्राधिकरण कानून की नीति घोषित करने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता क्योंकि यह विधायी निकाय की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, कानून के निर्बाध कार्यान्वयन में कार्यकारी प्राधिकरण, जिसे शक्तियां सौंपी गई हैं, की मदद करने वाले मानकों को निर्धारित करना भी विधानमंडल की जिम्मेदारी है।
मामले का विश्लेषण
न्यायालय किसी भी प्रत्यायोजित विधान की वैधता का निर्णय इस आधार पर कर सकता है कि वह मूल विधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अधिकार क्षेत्र से बाहर का सिद्धांत प्रशासनिक कानून के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। यह सिद्धांत यह प्रदान करता है कि किसी भी प्राधिकरण को अपने कार्यों का प्रयोग केवल उसी सीमा तक करने का अधिकार है, जिस सीमा तक उसे किसी कानून द्वारा प्रदान किया गया है। जब प्राधिकरण अपने प्रदत्त शक्ति के दायरे में अपने कार्यों का प्रयोग करता है, तो यह कहा जाता है कि प्राधिकरण की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है और पूरी तरह से वैध है। हालाँकि, जब कोई प्राधिकरण अपनी प्रदत्त शक्तियों की सीमा को पार कर जाता है, तो प्राधिकरण की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर कहलाती है। एक बार जब प्रत्यायोजित विधान को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर दिया जाता है, तो यह शून्य हो जाता है और इसलिए, लागू नहीं किया जा सकता है।
एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड, ब्यावर एवं अन्य बनाम अजमेर राज्य एवं अन्य (1954) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर चर्चा की थी कि ऐसे मामलों में जहां विधानमंडल को किसी विशेष विषय को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, वहां ऐसी शक्तियों के साथ-साथ नियम बनाने की भी एक निहित शक्ति होनी चाहिए। संवैधानिक कानून के प्राथमिक सिद्धांतों में से एक यह है कि शक्ति प्रदान करने में ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य सभी चीजें शामिल हैं। विधानमंडल को अपने आवश्यक विधायी कार्य से खुद को अलग करने और उसे किसी बाहरी प्राधिकरण को सौंपने का अधिकार नहीं है। विधानमंडल को कानून बनाने का प्राथमिक दायित्व दिया गया है, हालाँकि, प्रतिनिधिमंडल को सहायक उपाय के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है।
वसंतलाल मगनभाई संजनवाला (1960) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्यायोजित विधान किस सीमा तक अनुमेय (परमिसिबल) है, यह अब अच्छी तरह से तय हो चुका है। विधानमंडल को किसी भी परिस्थिति में अपने आवश्यक विधायी कार्य को सौंपने का अधिकार नहीं है। अपनी सहायक शक्तियों को सौंपने से पहले, विधानमंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने विधायी नीतियां और सिद्धांत प्रदान किए हैं। विधानमंडल का दायित्व है कि वह उक्त नीतियों और सिद्धांतों के निर्वहन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करे।
यहां तक कि जब विधानमंडल को अधिकार सौंपने का अधिकार दिया जाता है, तब भी उसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने चाहिए। इसी के मद्देनजर, हरकचंद रतनचंद बंथिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1969) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 की धारा 5(2)(b), जो सरकार को सोने के निर्माण, वितरण, उपयोग, निपटान, खपत आदि को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है, असंवैधानिक थी क्योंकि यह कोई पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने में विफल रही।
सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, त्रिवेंद्रम एवं अन्य बनाम के. कुंजाबमु एवं अन्य (1979) के मामले में अधिकार सौंपने की शक्ति पर चर्चा करते हुए कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं को संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। कानून बनाने की इस शक्ति में अधिकार सौंपने की शक्ति भी शामिल है। हालांकि, अत्यधिक अधिकार सौंपने का मतलब है अधिकार त्यागना। न्यायालय ने कहा कि असीमित अधिकार सौंपने से प्रतिनिधि अनियंत्रित तरीके से काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं या उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं।
जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एवं अन्य बनाम सुभाष चंद्र यादव एवं अन्य (1988) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई कानून नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है और उस शक्ति के बाद नियम बनाए गए हैं, तो ऐसे नियम कानून का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए, इन नियमों में वैधानिक बल है। हालांकि, इन नियमों को वैधानिक बल में रखने के लिए, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी
- नियम उस मूल कानून के अनुरूप होने चाहिए जिसके तहत इसे तैयार किया गया है;
- नियम बनाने वाले प्राधिकारी के पास नियम बनाने की शक्ति और अधिकार है।
नतीजतन, अगर कोई नियम इन दो शर्तों में से किसी के अनुरूप नहीं है, तो यह शून्य हो जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने उपभोक्ता कार्रवाई समूह एवं अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2000) के मामले में चर्चा की कि जब कोई कानून किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण को अधिकार सौंपने की शक्ति प्रदान करता है, चाहे उसका विवेक कितना भी व्यापक क्यों न हो, प्रतिनिधि को उन शक्तियों का प्रयोग तर्कसंगतता के दायरे में करना चाहिए और शक्ति के ऐसे प्रयोग को न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। सौंपी गई शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।
एक गतिशील समाज में विधायिका सभी बहुआयामी मुद्दों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकती। इसलिए, शासन के जटिल और विस्तृत पहलुओं को संभालने के लिए, नियम बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन अत्यंत आवश्यक है। यह प्रतिनिधिमंडल कार्यपालिका को मूल कानून के दायरे में नियम, उपनियम या विनियम बनाने का अधिकार देता है। हालांकि, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी की भावना भी जुड़ी होती है। इसलिए, नियम बनाने की शक्ति सौंपते समय, विधानमंडल को शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कड़े नियंत्रण प्रदान करने चाहिए। न्यायिक समीक्षा, संसदीय नियंत्रण, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय, समिति की निगरानी आदि कुछ सुरक्षा उपाय हैं जो सामूहिक रूप से सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्यायोजित विधान पारदर्शी है और मूल विधान के भीतर समाहित है।

निष्कर्ष
स्वतंत्रता के बाद के न्यायिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहाँ न्यायालयों ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग रुख अपनाया है। जहाँ कुछ मामलों में न्यायालयों ने विधानमंडल द्वारा अपनी शक्तियाँ सौंपने के कार्य का समर्थन किया है, वहीं अन्य मामलों में उन्होंने इस तरह के कदम के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
जिस तरह तलवार दोधारी हथियार है, उसी तरह प्रत्यायोजित कानून भी है। यह विधानमंडल के लिए ऐसे कठिन समय में वरदान साबित हो सकता है, जब वह सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से उत्पन्न गतिशील चुनौतियों का समाधान करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, लेकिन यह उन जगहों पर अभिशाप भी बन सकता है, जहां विधानमंडल अपनी सीमाओं को लांघ जाता है और अधिनियम की नीति को लागू करने के लिए आवश्यक सहायक कार्यों के बजाय आवश्यक विधायी कार्यों को सौंप देता है। इस तरह के प्रत्यायोजन की जब जांच नहीं की जाती है, तो कार्यपालिका को मनमाने ढंग से काम करने और लोकतंत्र के हर स्तंभ को सौंपी गई शक्तियों को असंतुलित करने की असीमित शक्तियाँ मिल सकती हैं।
यह ध्यान रखना चाहिए कि जब विधानमंडल कार्यपालिका को कुछ कार्य सौंपता है, जिन्हें कार्यपालिका की ओर से पूरा किया जाना चाहिए, तब भी कार्यपालिका कभी भी विधानमंडल के अधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकती या ऐसे मामलों में सर्वोच्च नहीं हो सकती। विधानमंडल के पास ऐसे प्रत्यायोजित विधान को जब भी वह उचित समझे, रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
आवश्यक विधायी कार्य क्या हैं?
मुख्य रूप से, आवश्यक विधायी कार्य विधानमंडल की मुख्य जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें किसी अन्य प्राधिकरण को नहीं सौंपा जा सकता है। कानून बनाना, नीति घोषित करना और बनाए गए कानूनों का ढांचा स्थापित करना आवश्यक विधायी कार्यों के कुछ प्रमुख तत्व हैं।
क्या आवश्यक विधायी कार्य विधानमंडल द्वारा सौंपे जा सकते हैं?
नहीं, विधानमंडल अपने आवश्यक विधायी कार्यों को किसी अन्य प्राधिकरण को नहीं सौंप सकता। हालाँकि, कुशल कार्यान्वयन के लिए, विधानमंडल द्वारा कुछ विनियामक या प्रशासनिक कार्यों को कार्यपालिका को सौंपा जा सकता है। सौंपते समय, विधानमंडल सौंपी गई शक्तियों पर कुछ दिशानिर्देश और सीमाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य है।
प्रत्यायोजन के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है?
प्रत्यायोजन के सिद्धांत का तात्पर्य केवल विधानमंडल से कार्यपालिका को विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन है। यह विधानमंडल को विधायी शक्तियों (आवश्यक विधायी कार्यों को छोड़कर) को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान बनाने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है। ये प्रत्यायोजित विधान आदेश, विनियमन या उपनियमों के रूप में हो सकते हैं। उचित प्रत्यायोजन के लिए, विधानमंडल मूल विधान के भीतर ही स्पष्ट मानकों और सीमाओं का प्रावधान करता है।
विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन से क्या महत्व जुड़ा है?
विधायिका के लिए भविष्य में परिस्थितियों में बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाली सभी जटिलताओं का पूर्वानुमान लगाना असंभव है। इस कमी को पूरा करने के लिए, विधानमंडल कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और बदलती परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ विधायी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है।
यह सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है कि विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन अनुमेय सीमाओं के भीतर हो?
न्यायिक समीक्षा एक शक्तिशाली तंत्र है जिसके माध्यम से न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच और संतुलन बनाए रखती है कि विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन अनुमेय सीमाओं के दायरे में आता है। जब भी न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी प्रत्यायोजन की वैधता को चुनौती देने वाला कोई मामला आता है, तो न्यायालय कानूनों को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय लेते हैं।
क्या प्रत्यायोजित कानून की वैधता को चुनौती देना जायज़ है?
हां, प्रत्यायोजित विधान को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मूल विधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चुनौती के अन्य आधार हैं प्रत्यायोजित विधान का अनुचित या मनमाना होना, प्रक्रियागत अनुचितता और सुरक्षा उपायों का अभाव होना।
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और प्रत्यायोजित विधान के बीच क्या संबंध है?
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल और कार्यपालिका के कार्यों के बीच उचित जाँच और संतुलन हो। यह आवश्यक विधायी कार्यों के परित्याग को रोकता है। यह न्यायपालिका को प्रत्यायोजित विधान के दायरे की समीक्षा करने के लिए कोई भी सुरक्षा उपाय करने का अधिकार देता है।
विधायी शक्तियों का समुचित हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए विधानमंडल द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं?
विधायी शक्तियों का उचित प्रत्यायोजन सुनिश्चित करने के लिए, विधानमंडल कार्यक्षेत्र, प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश और नीतिगत उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है। विधानमंडल समय-समय पर नियमों की समीक्षा कर सकता है और शक्ति के दुरुपयोग के मामले में प्रत्यायोजित विधान को रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति भी सुरक्षित रख सकता है।
क्या कार्यपालिका को प्रत्यायोजित शक्ति के अंतर्गत नया कानून बनाने का अधिकार है?
कानून बनाना विधानमण्डल के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, कार्यपालिका प्रत्यायोजित शक्ति के तहत नया कानून नहीं बना सकती। कार्यपालिका केवल मूल कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम और विनियम बना सकती है।
जब न्यायालय किसी प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक घोषित कर देता है तो क्या होता है?
एक बार जब न्यायालय पाता है कि प्रत्यायोजित विधान असंवैधानिक है, तो वह प्रत्यायोजित विधान को रद्द कर सकता है। न्यायालय को यह तय करने का अधिकार है कि प्रत्यायोजित विधान को अमान्य करने का प्रभाव पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) होगा या नहीं। न्यायालय उन लोगों के पक्ष में कुछ उपाय भी प्रदान कर सकता है जो आक्षेपित प्रत्यायोजित विधान से प्रभावित हुए हैं।
प्रत्यायोजित विधान के उदाहरण क्या हैं?
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को अधिनियम के दायरे में विनियमन बनाने का अधिकार देती है, ताकि इसके उचित क्रियान्वयन को प्रभावी बनाया जा सके।
विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन और विधायी शक्ति के त्याग के बीच बुनियादी अंतर क्या हैं?
विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन और विधायी शक्ति के त्याग के बीच मूल अंतर यह है कि विधानमंडल द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया पर कितना नियंत्रण रखा जाता है। आवश्यक विधायी कार्य को छोड़कर विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन अनुमत है। हालाँकि, जब विधानमंडल अपने आवश्यक विधायी कार्य को कार्यपालिका को हस्तांतरित करता है, तो यह विधायी शक्ति का त्याग होता है, जो असंवैधानिक है।
भारत में विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजन के सिद्धांत के ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?
भारत में प्रत्यायोजन के सिद्धांत से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित हैं:
- दिल्ली कानून अधिनियम, 1932, अजमेर-मेरवाड़ा (विस्तार) बनाम भाग सी राज्य (कानून) अधिनियम, 1950 (1951)
- हमदर्द दवाखाना (वक्फ) लाल कुआं, दिल्ली एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (1959)
- हरिशंकर बागला एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1954)
संदर्भ
- https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/Administrative-Law-and-Doctrine-of-Excessive-Delegation.pdf







