यह लेख Harshita Agrawal द्वारा लिखा गया है। यह लेख कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए गहन निष्कर्षों और ऐतिहासिक फैसलों को निर्दिष्ट करता है। लेख में अंतर्निहित प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तर्कों के साथ-साथ तथ्यात्मक पृष्ठभूमि, कानूनी तर्क और निर्णय की जटिलताओं पर भी गहन चर्चा की गई है। यह महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों और उसके बाद अदालत के फैसले के बाद कानून से जुड़े विभिन्न बयानों और तर्कों पर भी प्रकाश डालता है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राथमिक कानून बनाने की शक्ति विधायिका में निहित है न कि कार्यपालिका में, लेकिन यह संभव है कि जब विधायिका काम नहीं कर रही हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों तो तत्काल कार्रवाई की जाए और तत्काल समाधान के लिए कानून बनाने में विधायिका की असमर्थता के कारण सार्वजनिक हित को होने वाले किसी भी नुकसान को रोका जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 क्रमशः के तहत अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी करने की शक्ति निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी समय अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की शक्ति होगी, जब इस विषय पर तुरंत संसदीय अधिनियम बनाना संभव न हो। अनुच्छेद 213 के तहत दी गई अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के समान है और राज्य विधानमंडल द्वारा एक अधिनियम के रूप में समकक्ष कानूनी अधिकार रखती है। राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल या दोनों सदनों में से कोई भी सत्र में नहीं हो। अध्यादेश केवल केंद्रीय मंत्रियों की सिफारिश पर ही जारी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि भारतीय संविधान की समवर्ती, संघ और राज्य सूची में उल्लिखित शक्ति का प्रसार किया जा सकता है। इस लेख का उद्देश्य उन स्थितियों और घटनाओं को निर्दिष्ट करना है जो तब संबोधित होती हैं जब कोई अध्यादेश बनाया जाता है और उसी नियम के अनुसार कानून लागू होता है लेकिन जब यह लागू नहीं होता है और कानून अभी भी वैध है। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) के मामले में इसे स्पष्ट करता है।
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) का विवरण
मामले का नाम
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य
न्यायालय का नाम
सर्वोच्च न्यायालय
फैसले की तारीख
2 जनवरी 2017
उद्धरण
(2017) 3 सर्वोच्च न्यायालय मामले (एससीसी) 1
पीठ
न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर (सहमत), न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर (असहमति), न्यायमूर्ति एस. ए.बोबडे (बहुमत),न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (बहुमत), न्यायमूर्ति उदय यू. ललित (बहुमत), न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ (बहुमत), न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव ( बहुमत)

लेखक
न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़
पक्षों का नाम
अपीलकर्ता: कृष्ण कुमार सिंह
प्रतिवादी: बिहार राज्य
मामले में शामिल कानून
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017), के मामले में कई कानून शामिल थे जो मामले में संबंधित विशेष कानूनी मुद्दों पर निर्भर थे। भारत में सरकारी कार्यों, अध्यादेशों और संवैधानिक मामलों से संबंधित मामलों में आमतौर पर उद्धृत कुछ प्रासंगिक क़ानून में शामिल हैं:
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 123, 133, 213 और 356
- बिहार शिक्षा संहिता,1961
मामले की पृष्ठभूमि
2 जनवरी, 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) मामले में अपना फैसला सुनाया। बिहार सरकार ने “बिहार राज्य गैर-सरकारी संस्कृत शैक्षणिक संस्थान (प्रशासन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अध्यादेश” 1989 में अधिनियमित किया। मामला अध्यादेश की वैधता या कार्यान्वयन पर सवाल उठाने वाली कानूनी चुनौतियों से उत्पन्न हो सकता है, जिसमें संभावित रूप से संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून और शिक्षा नीति से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। कानूनी कार्यवाही में अध्यादेशों को लागू करने के राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार, ऐसे उपायों को लागू करने के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और प्रभावित शैक्षणिक संस्थानों के निहितार्थ से संबंधित तर्क और विचार-विमर्श शामिल थे। इस अधिनियम का उद्देश्य 429 निजी संस्कृत शिक्षण संस्थानों को राज्य के नियंत्रण में लाना और स्कूल में पेशेवरों की नियुक्ति पर बिहार का अधिकार क्षेत्र प्रदान करना था। इस प्रारंभिक अध्यादेश के बाद, कई अन्य को विधायी निकाय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए बिना अधिनियमित किया गया और इस प्रकार कानून बनने में विफल रहे। पिछला अध्यादेश बंद होते ही नया अध्यादेश तुरंत लागू कर दिया गया। अंततः, मामले का फैसला न्यायपालिका द्वारा किया गया होगा, जिसमें संभवतः विभिन्न अदालती स्तरों पर कार्यवाही शामिल होगी, जिसका बिहार में निजी शैक्षणिक संस्थानों के शासन और निरीक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) के तथ्य
यह मामला एक अध्यादेश को दोबारा जारी करने की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है। 1989 में, बिहार सरकार ने बिहार गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अध्यादेश (1989) नामक एक अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश के अनुसार, 429 संस्कृत विद्यालय जो निजी तौर पर नियंत्रित थे, उन्हें अब बिहार सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाएगा, जिससे उन विद्यालयों के कर्मचारियों और शिक्षकों को स्थानांतरित कर सरकारी कर्मचारी और शिक्षक बना दिया जाएगा। पहले अध्यादेश के बाद अन्य अध्यादेशों का क्रम जारी रहा और इन अध्यादेशों से संबंधित कोई भी कानून कभी पारित नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें से कोई भी राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।
परिणामस्वरूप,उन्होंने अपने वेतन और अन्य देय राशि के भुगतान के लिए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, इस आधार पर कि वे अब अध्यादेश संख्या 1989 का 32 के लागू होने के प्रभाव से सरकारी कर्मचारी हैं, और उसके बाद भी वे ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि अध्यादेश की वैधता 30 अप्रैल 1992 तक है।
पटना उच्च न्यायालय का फैसला
इस मामले में, पटना उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित मुख्य मुद्दा अध्यादेशों की पुन: घोषणा की कानूनी और संवैधानिक वैधता थी। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्थापित करते हुए याचिका खारिज कर दी कि पर्याप्त औचित्य के बिना पुन: जरी करना कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986) मामले को अदालत में ले जाया गया और पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संवैधानिकता के मौलिक सिद्धांतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि 305 स्कूल वास्तव में अध्यादेश की वैधता के अंतिम दिन 30 अप्रैल 1992 तक वेतन प्राप्त करने के हकदार थे। इसके अतिरिक्त, निजी स्कूलों के सभी प्रबंधन पहले अध्यादेश के लागू होने से पहले उसी नियामक ढांचे द्वारा शासित होंगे। हालांकि, डी. सी. वाधवा के फैसले का दोष यह है कि संवैधानिक सिद्धांत की व्याख्या करने के बाद, संवैधानिक पीठ केवल ‘आशा और विश्वास’ के साथ समाप्त हुई कि अध्यादेशों की पुन: घोषणा के माध्यम से कानून बनाना आदर्श नहीं बनेगा। बाद के मामलों में बार-बार जारी किए गए अध्यादेशों से यह भरोसा झूठा साबित हुआ है। अंतिम निर्देश मध्यवर्ती शिक्षा के संबंध में एक अध्यादेश जो प्रभावी रहा उसको अमान्य करना था। विशेष रूप से, डी. सी. वाधवा का मामला उन अध्यादेशों के तहत की गई कार्रवाइयों की कानूनी स्थिति से नहीं निपटा, जो समाप्त हो चुके हैं या अस्वीकार कर दिए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में अपील: दो न्यायाधीशों की पीठ
उपरोक्त आदेश के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर और न्यायमूर्ति डी. पी. वाधवा की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने यह भी माना कि बिहार के राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को फिर से जारी करना स्पष्ट रूप से संसद की संवैधानिकता का उल्लंघन है। हालांकि, पहले अध्यादेश की वैधता के संबंध में उनकी राय अलग-अलग थी। इस मामले में प्रारंभिक अध्यादेश बिहार गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) अध्यादेश, 1989 है, जिसे 1989 के अध्यादेश 32 के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 651 निजी संस्कृत विद्यालयों में से 429 पर नियंत्रण लेने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस असहमति के कारण मामला उच्च प्राधिकारी को भेजा गया जिसके परिणामस्वरूप तीन न्यायाधीशों वाली पीठ को अपील की गई। संविधान में ढांचे का उल्लेख करते हुए, संविधान पीठ ने कहा कि अध्यादेश की वास्तविक प्रक्रिया क्या है और अध्यादेश को लागू करने की शक्ति अनिवार्य रूप से असाधारण स्थितियों में मिलने की शक्ति है और इसे “राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकृत” करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। खंड पीठ द्वारा दिए गए फैसले में यह भी उल्लेख किया गया था कि संविधान में विधायिका को विधायी कार्य सौंपा है जिसमें लोगों के प्रतिनिधि शामिल हैं और यदि कार्यपालिका को विधायी जांच के अधीन हुए बिना पुन: प्रख्यापित के माध्यम से अध्यादेशों के प्रावधानों को बनाए रखने की अनुमति दी जाती है तो अधिकारियों द्वारा कानून का उल्लंघन होगा। कार्यपालिका आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि वह केवल तभी लागू होती हैं जब संसद काम नहीं कर रही हो। इस तरह की कार्रवाइयां हमारे संवैधानिक ढांचे में निहित लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से कमजोर कर देंगी।

तीन न्यायाधीशों की पीठ का हवाला
हालांकि, दो-न्यायाधीशों की पीठ की पहले अध्यादेश की वैधता पर राय में अंतर के कारण, राय को संतुलित करने और उल्लिखित तथ्यों और मामले की कानूनी वैधता की समीक्षा करने के बाद मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया था। इसे फिर से बड़ी पीठ को भेजा गया।
पांच न्यायाधीशों की पीठ का हवाला
वर्ष 1999 में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इसे पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया क्योंकि इसने संविधान और अध्यादेश की पुन: घोषणा की वैधता के बारे में पर्याप्त प्रश्न उठाए थे क्योंकि न्यायिक समीक्षा के लिए विधायिका के समक्ष रखे बिना कई बार पुन: प्रख्यापित किया गया था।
सात न्यायाधीशों की पीठ का हवाला
23 नवंबर 2004 को मामला सात न्यायाधीशों की बेंच को भेजा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा 2 जनवरी, 2017 को दिए गए फैसले में अध्यादेशों की घोषणा को संविधान का उल्लंघन और लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रियाओं को कमजोर करने का एक साधन माना गया। अदालत ने यह भी घोषित किया कि जहां भी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का निर्णय लेते हैं, वे न्यायिक जांच से मुक्त नहीं होंगे।
सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष उठाए गए मुद्दे
- क्या उक्त अध्यादेश के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व उसके लागू होने के समाप्त होने के बाद भी मौजूद हैं या नहीं?
- क्या संविधान के अनुसार कोई अध्यादेश दोबारा जारी किया जा सकता है या नहीं?
- क्या अधिकारियों के लिए अध्यादेशों को न्यायिक जांच के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है या नहीं?
- क्या पुन: प्रख्यापन की प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध थी और बिहार के राज्यपाल द्वारा इसका पालन किया गया था या नहीं?
- क्या अध्यादेश बनाने की शक्ति का अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया गया था या नहीं?
- क्या अध्यादेश समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता किसी कानूनी अधिकार के हकदार थे या नहीं?
- क्या अध्यादेश रद्द होने के बाद इसके तहत कोई सजा का प्रावधान है या नहीं?
पक्षों की दलीलें
उल्लिखित मामले में पक्षों के बीच असहमति का मुख्य मुद्दा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उनके संबंधित अनुच्छेदों के तहत जारी किए गए अध्यादेशों की घोषणा और पुनः घोषणा की संवैधानिक वैधता थी।
याचिकाकर्ता
दिए गए मामले में याचिकाकर्ता अध्यादेशों के आधार पर राहत की मांग कर रहे थे। उन्होंने उक्त अध्यादेश द्वारा उन्हें दिए गए ‘सरकारी कर्मचारियों’ के रूप में वर्गीकरण का हवाला देते हुए, सरकार से वेतन और अन्य लाभों का दावा करने के अपने अधिकार को माननीय न्यायालय के ध्यान में लाया।
उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि वे पहले अध्यादेश की घोषणा के दिन से सरकार से वेतन और लाभ प्राप्त करने के हकदार थे और अंतिम अध्यादेश को लागू होने के समय के बाद भी लाभ प्राप्त करना जारी रखना चाहिए।
प्रतिवादी
प्रतिवादी ने उस तारीख से पहले एक अध्यादेश के तहत की गई कार्रवाइयों की वैधता और परिणामों के बारे में दावा उठाया, जब विधान सभा द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद इसे ‘संचालन बंद’ करने के लिए कहा जाता है।
दलीलों में कहा गया कि चूंकि अध्यादेश अमान्य थे, इसलिए वे उक्त स्कूलों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोई वेतन या लाभ देने के लिए बाध्य नहीं थे।

कानूनों पर चर्चा हुई
संविधान का अनुच्छेद 123
यह संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बताता है। जब संसद अत्यावश्यक मामलों को संबोधित करने के लिए काम नहीं कर रही हो तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति की इस अध्यादेश बनाने की शक्ति का दायरा संसद की विधायी शक्तियों के साथ सह-व्यापक है, अर्थात यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है और यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान ही संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।
अध्यादेश बनाते समय कुछ विशिष्टताओं का पालन किया जाना चाहिए:
- राष्ट्रपति को यह शक्ति तभी प्राप्त होती है जब संसद के दोनों सदन काम नहीं कर रहे हों और संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता हो।
- राष्ट्रपति द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग केवल अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से किया जाता है।
- अध्यादेश को संसद के पुन: एकत्र होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए और पुन: संयोजन की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या अध्यादेश को अस्वीकार करने वाले संकल्प पारित होने से पहले स्वचालित रूप से प्रभावी होना बंद हो जाएगा। यदि सदन अलग-अलग तारीखों पर दोबारा एकत्रित होते हैं तो छह सप्ताह की अवधि बाद की तारीख से गिनी जाएगी।
- राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है।
आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ (1982) में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की समान शक्ति का जिक्र करते हुए, इस अदालत की एक संवैधानिक पीठ ने कहा कि प्रारंभिक जांच पर, यह असामान्य लग सकता है कि कानून बनाने का अधिकार संविधान निर्माताओं द्वारा सौंपा गया था। परंपरागत रूप से, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक ढांचे के भीतर, विधायी शक्ति को विशेष रूप से लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से संबंधित माना जाता है और इसे विधायिका के प्रति जिम्मेदारी के माध्यम से कार्यपालिका में निहित करना अलोकतांत्रिक होगा क्योंकि यह कार्यपालिका को इस अधिकार का दुरुपयोग करने में सक्षम बना सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 133
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 133 के अनुसार नागरिक मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल कार्यवाही में जारी किए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134A के तहत प्रमाणित करे।
- यह मामला सामान्य महत्व के कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है?
- उच्च न्यायालय के विचार में, उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता है?
प्रावधानों के बावजूद अनुच्छेद 132 खण्ड (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने वाला कोई भी पक्ष, अन्य आधारों के अलावा, यह दावा कर सकता है कि संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का गलत निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, इस अनुच्छेद की सामग्री के बावजूद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा निर्धारित न करे।
इस अनुच्छेद का एक उदाहरण रमेश बनाम गेंदालाल मोतीलाल पाटनी (1966) के ऐतिहासिक फैसले में पाया जा सकता है, जहां बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई। फैसले के तहत, एक दावा अधिकारी ने यह कहते हुए आरोपों को खारिज कर दिया कि यद्यपि ऋण एक डिक्री में विलय हो गया था, इसे एक सुरक्षित ऋण माना जाएगा और राशि भी वसूली योग्य थी। इसके अलावा, अधिकारी ने दावे का विवरण मांगा लेकिन इसके बजाय, प्रतिवादी ने समिति के समक्ष मुख्य आदेश के खिलाफ अपील दायर की। समिति ने माना कि ऋण की प्रकृति निर्धारित करना दावा अधिकारी के हाथ में नहीं है और केवल सिविल न्यायालय ही इस मुद्दे पर निर्णय ले सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 213
इसमें विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। यदि किसी भी समय, सिवाय इसके कि जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में हो, या जहां एक राज्य में विधान परिषद है, सिवाय जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हों, राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसे तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वह ऐसे अध्यादेश जारी कर सकता है जैसा कि परिस्थितियाँ उसे आवश्यक प्रतीत होती हैं।
बशर्ते कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के निर्देश के बिना, ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि-
- यदि संविधान के समान प्रावधानों वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- उन्होंने राष्ट्रपति के विचार के लिए समान प्रावधानों वाले विधेयक को आरक्षित करना आवश्यक समझा होगा।
- इस संविधान के तहत समान प्रावधानों वाला राज्य विधानमंडल का एक अधिनियम राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होने के कारण अमान्य हो जाएगा, इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई थी।

अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुन: संयोजन होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए और पुन: संयोजन की तारीख से छह सप्ताह की समाप्ति पर स्वचालित रूप से प्रभावी होना बंद हो जाएगा जब तक कि विधानमंडल द्वारा पहले इसे अस्वीकार न कर दिया गया हो।
उपरोक्त अनुच्छेद की क्रियाशीलता का प्रदर्शन ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1982) मे ऐतिहासिक निर्णय में पाया जा सकता है। जहां अनुच्छेद 213 के तहत यह दृढ़ता से स्थापित किया गया था कि एक अध्यादेश एक कानून है और इसे केवल एक की तरह ही माना जाना चाहिए। हमारे संविधान के तहत विधायी कार्रवाई कुछ सीमाओं के अधीन है और विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून और पारित होने में अक्षम होने पर संविधान के भाग तीन का उल्लंघन होगा। किसी क़ानून को पारित करने में विधायिका का मकसद अदालतों की जांच से परे है और अदालत को मंजूरी देने से पहले इसके प्रावधान की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी विधायी अधिनियम की आवश्यकता और आपात स्थिति केवल विधायी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है, न्यायालय द्वारा नहीं। अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत पारित अध्यादेश इन्हीं आधारों पर खड़ा होता है। किसी अध्यादेश को प्रशासनिक निर्णय नहीं माना जा सकता और भारतीय संविधान के तहत इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं।
संविधान का अनुच्छेद 356
भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के टूटने की स्थिति में, यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राज्य सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है, तो राष्ट्रपति एक उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) जारी कर सकता है-
- राज्य सरकार के कुछ या सभी कार्यों के साथ-साथ राज्यपाल या राज्य विधानमंडल को छोड़कर किसी भी राज्य निकाय या प्राधिकरण में निहित या प्रयोग करने योग्य शक्ति को मानें।
- घोषणा करें कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा।
- उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक या वांछनीय समझे जाने वाले किसी भी अतिरिक्त प्रावधानों को अधिनियमित करें, जिसमें राज्य निकायों या प्राधिकरणों से संबंधित किसी भी संवैधानिक प्रावधान को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित करना भी शामिल है।
बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या प्रयोग की जाने वाली किसी भी शक्ति को स्वयं ग्रहण करने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, ना ही यह उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने की अनुमति देता है। ऐसी किसी भी उद्घोषणा को बाद की उद्घोषणा द्वारा निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है और इस अनुच्छेद के तहत जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। जब तक कि यह पिछली घोषणा को रद्द करने वाली उद्घोषणा न हो, यह दो महीने के बाद प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उक्त अवधि समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदनों में पारित प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न हो जाए।
बशर्ते कि यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (पिछली उद्घोषणा को रद्द करने वाली उद्घोषणा न हो) तब जारी की जाती है जब लोक सभा भंग हो जाती है या यदि इसका विघटन उपरोक्त दो महीने की अवधि के दौरान होता है, और यदि राज्यों की परिषद इसे मंजूरी देते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है लेकिन उक्त अवधि की समाप्ति से पहले लोक सभा द्वारा इसके संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है, तो लोक सभा के पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठने के तीस दिन बाद उद्घोषणा प्रभावी नहीं रहेगी, जब तक कि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।
बशर्ते कि एक उद्घोषणा जिसे मंजूरी दे दी गई है, उसके जारी होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगी जब तक कि उससे पहले रद्द न कर दी जाए।
बशर्ते कि यदि ऐसी उद्घोषणा के लागू बने रहने को मंजूरी देने वाला कोई प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है, तो उद्घोषणा उस तारीख से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक कि वह इस खंड के तहत समाप्त न हो जाती है, जब तक उसे वापिस ना लिया जाए। ऐसी कोई भी उद्घोषणा किसी भी परिस्थिति में तीन साल से अधिक समय तक वैध नहीं रहेगी।
बशर्ते कि यदि लोकसभा किसी छह महीने की अवधि के दौरान भंग हो जाती है और यदि राज्य परिषद ऐसी उद्घोषणा को जारी रखने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन उस अवधि के दौरान लोक सभा द्वारा इसकी निरंतरता के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है तब उद्घोषणा लोक सभा के पुनर्गठन के बाद पहली बार बैठने के तीस दिन बाद प्रभावी नहीं रहेगी जब तक कि उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर लोक सभा द्वारा उद्घोषणा को जारी रखने का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाता।
रंग रूपी विधान का सिद्धांत
“रंग रूपी विधान का सिद्धांत” (कलरेबल लेजिस्लेशन) यह एक कानूनी सिद्धांत है, इसका उद्देश्य सरकार के विधायी अधिकार के असंवैधानिक उपयोग को रोकना है। यदि विधायिका को कुछ करने से प्रतिबंधित किया गया है, तो उसे किसी भी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए या कानूनी वैधता के भीतर कार्य करने का दिखावा नहीं किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत इस कहावत से उपजा है कि ‘जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। हालांकि, एक विधायिका किसी कानून को इस तरह से पारित कर सकती है कि वह संवैधानिक लगे द, जबकि वास्तव में, उस कानून का उद्देश्य कुछ ऐसा हासिल करना है जो विधायिका ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह के कानून को रंग रूपी कानून कहा जाता है और यह अमान्य है।
एक उदाहरण लेने के लिए कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य (1952), का मामला है जिसमे बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 में प्रावधान किया गया कि किरायेदारों द्वारा अवैतनिक (अनपैड) किराया राज्य में निहित होगा और उनमें से आधा राज्य द्वारा अवैतनिक लगान के अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में मकान मालिक या जमींदार को वापस भुगतान किया जाएगा। राज्य सूची के एक प्रावधान के अनुसार जिसके तहत उपरोक्त कानून पारित किया गया था, मुआवजे के भुगतान के बिना कोई संपत्ति अर्जित नहीं की जानी चाहिए। सवाल यह था कि क्या पूरे अवैतनिक किराए को लेना और फिर उसका आधा हिस्सा उन लोगों को वापस लौटा देना जो दावा करने के हकदार थे, एक ऐसा कानून है जो मुआवजे का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि यह राज्य विधानमंडल द्वारा अधिग्रहण की शक्ति का एक रंग रूपी अभ्यास था, क्योंकि “पूरा लेने और आधा वापस करने का मतलब बिना किसी वापसी के बात करने से ज्यादा या कम कुछ नहीं है और यह नग्न जब्ती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यह किसी भी विशिष्ट रूप में पहना या प्रच्छन्न हो सकता है। अधिकारियों का दायित्व है कि वे अपनी स्थिति को सम्मानजनक तरीके से बनाए रखें और निर्णय जनता की आकांक्षाओं पर आधारित होने चाहिए। न्यायपालिका के पास सत्ता के सरकारी दुरुपयोग को रोकने का अधिकार है। जब सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से परे कानून बनाकर अपनी विधायी शक्ति का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका इन कानूनों की जांच करने और असंवैधानिक पाए जाने पर उन्हें रद्द करने की शक्ति रखती है।
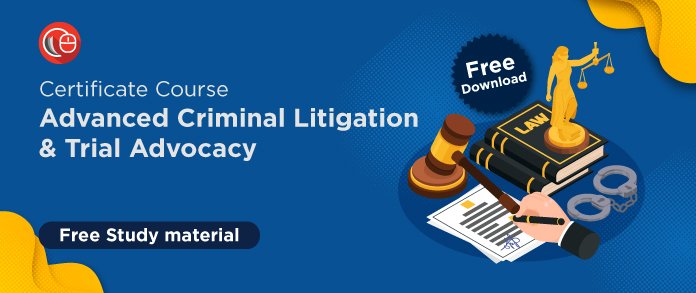
2017 में मामले का अंतिम फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया है और अध्यादेशों को फिर से जारी करने की संवैधानिक वैधता से संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने 5:2 के अनुपात में कहा कि बिना किसी सीमा के अध्यादेश दोबारा जारी करना असंवैधानिक है। उपरोक्त मामले में, पीठ ने घोषणा की कि अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई शक्तियों को न्यायिक समीक्षा से छूट नहीं है। यह निर्णय न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति बोबडे, न्यायमूर्ति ललित, न्यायमूर्ति गोयल और न्यायमूर्ति नागेश्वर राव के साथ स्वयं की ओर से लिखा था, जिसमें कहा गया था कि संविधान कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन यह एक सशर्त विधायी शक्ति है। इसका प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। अदालत ने फैसले डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, (1986) के महत्व पर भी प्रकाश डाला जहां अध्यादेशों को दोबारा जारी करना संविधान का उल्लंघन माना गया।
सहमत राय
तब मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने सहमति व्यक्त की और विधायिका के समक्ष अध्यादेश पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 द्वारा लगाए गए दायित्वों के संबंध में एक प्रासंगिक प्रश्न उठाया। यह अवलोकन संवैधानिक प्रावधानों की प्रकृति की जटिलता को रेखांकित करता है जो आगे की न्यायिक जांच की आवश्यकता का संकेत देता है।
असहमति राय
असहमति पूर्ण राय देते हुए न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने निम्नलिखित कहा-
- अनुच्छेद 213 विधायिका के समक्ष अध्यादेश प्रस्तुत करने का आदेश नहीं देता है।
- चूँकि एक अध्यादेश एक कानून का महत्व रखता है, इसलिए इसकी वैधता इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि इसे विधायिका के समक्ष पेश किया गया था या नहीं।
- अध्यादेश, चाहे वह विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 213(2)(a) के प्रावधानों के अनुसार और विधान सभा द्वारा ही निर्धारित किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 213(2)(B) के तहत अध्यादेश के लागू होने के बाद उसके भाग्य पर कार्यपालिका का अधिकार किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा उसे वापस लेने तक सीमित है और अधिकांश नियंत्रण राज्य विधानमंडल के पास है, जो राज्य के प्राथमिक विधायी निकाय के रूप में कार्य करता है।
इस फैसले के पीछे तर्क
अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देते हैं। जब संसद नहीं चल रही हो तो अध्यादेश सरकार को तत्काल विधायी उपाय करने का अधिकार देता है। इन कार्यकारियों की शक्तियों को न्यायिक समीक्षा से छूट नहीं दी गई है और विधायी जांच के समक्ष रखे बिना अध्यादेशों को फिर से जारी करना लोकतांत्रिक विधायी प्रक्रिया को कमजोर करता है। यद्यपि अध्यादेश को कानून के समकक्ष माना जाता है, यह राष्ट्रपति/राज्यपाल को स्वतंत्र विधायी अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 213 विधायिका के समक्ष अध्यादेश पेश करने के लिए कार्यपालिका पर एक अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य लगाता है। यह अनिवार्य है क्योंकि विधायिका को यह निर्धारित करना है:
- अध्यादेश प्रख्यापित करने की आवश्यकता है ।
- क्या अध्यादेश को मंजूरी दी जानी चाहिए या खारिज करना चाहिए?
- क्या अध्यादेश के प्रावधानों को शामिल करने वाला अधिनियम बनाया जाना चाहिए?
डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, (1986) के निर्णय में न्यायालय द्वारा कहा गया कि किसी अध्यादेश को दोबारा जारी करना असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 जो अध्यादेश जारी करने की प्रतिबंधात्मक शक्ति को रेखांकित करते है के इरादे को कमजोर करता है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अध्यादेश का प्रभाव अपरिवर्तनीय होना चाहिए और उक्त अध्यादेश को जारी रखने को उचित ठहराना जनता के हित में होना चाहिए। न्यायालय को शक्ति के प्रयोग की वैधता निर्धारित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांत के अनुरूप, अध्यादेशों की शक्ति विधायी निरीक्षण के अधीन है, और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जवाबदेह है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के तहत जारी किया गया अध्यादेश विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही शक्ति और प्रभाव रखता है, यदि इसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और विधायिका के पुनः एकत्रित होने के छह सप्ताह बाद या इससे पहले इसे अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित होने पर यह काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एक अध्यादेश को भी रद्द किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल को एक अलग विधायी निकाय या कानून बनाने के स्वतंत्र स्रोत के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं देती है।
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) में संदर्भित ऐतिहासिक मामले
कुछ ऐतिहासिक निर्णय हैं जो वर्तमान मामले के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए एक संदर्भ साबित हुए हैं। नीचे उल्लिखित मामलो ने प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के दुरुपयोग और उसके बाद उल्लिखित अदालत के फैसले पर प्रकाश डाला। अध्यादेश एक कानून है जिसे इसी तरह माना जाना चाहिए। हालांकि, जिनके पास अध्यादेशों को जारी करने और दोबारा लागू करने की शक्ति है, उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद के समक्ष पेश करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि अध्यादेशों को फिर से जारी करने के अधिकार का उपयोग वास्तविक तरीके से किया जाए और अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग न किया जाए।
डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986)
डी. सी. वाधवा एक प्रोफेसर थे और उनके पास विभिन्न अध्यादेशों को फिर से जारी करने की राज्यपाल की शक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका थी। व्यापक शोध के बाद, उन्होंने बिहार के राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के दुरुपयोग का पता लगाया क्योंकि सरकार द्वारा कानून पर विचार किए बिना या अध्यादेश में एक भी बदलाव किए बिना एक से चौदह वर्षों के बीच 256 अध्यादेश फिर से जारी किए गए थे। तर्क यह है कि प्रतिवादी एक बाहरी व्यक्ति है जिसका अध्यादेशों की वैधता में कोई कानूनी हित नहीं है और इस प्रकार उसे रिट याचिका में कुछ कहने या न कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके तर्क में यह भी उल्लेख किया गया था कि अध्यादेशों को उनकी संवैधानिक वैधता के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है और शेष अध्यादेश संसद में अधिनियम बनने की राह पर हैं।

मामले के फैसले से पता चलता है कि चूंकि राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को फिर से जारी करना इसे असंवैधानिक बनाने वाली शक्ति का एक रंग रूपी अभ्यास माना जाएगा। माननीय न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि कानून संविधान के अनुसार बनाये जाते हैं न कि कार्यपालिका की शक्ति से।
भूपेन्द्र कुमार बोस बनाम ओडिशा राज्य (1962)
भूपेन्द्र कुमार बोस बनाम ओडिशा राज्य (1962) के ऐतिहासिक फैसले में अधिकार का दावा करने का सिद्धांत स्थापित किया गया था जो एक अनंतिम (प्रोविजनल) अधिनियम के सादृश्य (एनालॉजी) पर आधारित है। इस मामले के तहत उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि दावों और आपत्तियों में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप सभी योग्य मतदाताओं की आयु प्रकाशित नहीं हो सकी।
उच्च न्यायालय ने दावा किया कि दावों और आपत्तियों को दाखिल करने में अवधि के इस भारी भ्रम ने चुनाव के परिणामों को सीधे प्रभावित किया है, और कई पात्र मतदाताओं के अधिकारों को वंचित कर दिया है जिनके योगदान के कारण परिणाम में बदलाव की कोई संभावना थी। यह स्पष्ट रूप से उड़ीसा नगर निगम के अधिकार द्वारा शक्ति का दुरुपयोग था क्योंकि उन्होंने केवल 14 दिनों की अवधि अधिसूचित की थी जबकि उम्मीदवार के पास प्रचार के लिए 15 दिन थे।
उच्च न्यायालय की नजर में याचिकाकर्ता इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहे कि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन किसी भी तरह से परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा का उचित आदेश पारित किया गया है। हालांकि, यहाँ दिया गया निर्णय एक सीमित दायित्व साबित हुआ और व्यापक रूप से प्रभावशाली नहीं माना गया।
टी. वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1985)
टी. वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1985), के मामले में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक अध्यादेश कानून के बराबर है और इसे प्रशासनिक कार्रवाई या अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय नहीं माना जा सकता है।
यह मामला भी इसी मामले की तरह एक अनंतिम अधिनियम की सादृश्यता अपनाने के अधिकार पर जोर देता है। भूपेन्द्र कुमार बोस बनाम ओडिशा राज्य (1962) में शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि जब संविधान अध्यादेश जारी करने की शक्ति निर्धारित करता है, तो इसे एक अधिनियम के बराबर माना जाएगा और इसमें एक विधायी अधिनियम की सभी विशेषताएं होनी चाहिए जिसमें संविधान में उल्लिखित अधिकार, सुरक्षा और बाधाएं शामिल हैं।
एस. कृष्णन बनाम मद्रास राज्य (1951)
एस. कृष्णन बनाम मद्रास राज्य (1951) के ऐतिहासिक फैसले के संदर्भ में, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा तर्क प्रस्तुत करने की इच्छा नहीं थी, और दावे का समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रशिक्षकों की स्थिति समाप्त कर दी गई थी और व्याख्याता (लेक्चरर) की भूमिका को प्रवेश स्तर की स्थिति के रूप में नामित किया गया था। इसलिए, अदालत की राय है कि प्रतिवादी के दावे को मंजूरी देने से कोई वैध उद्देश्य पूरा नहीं होगा और लाभ के वितरण के संबंध में भ्रम पैदा हो सकता है।
उपरोक्त मामले के कानून के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर विचार करते हुए, अदालत रिट अपील को स्वीकार करती है और रिट याचिकाओं को खारिज कर देती है। परिस्थितियों को देखते हुए, किसी भी पक्ष को लागत वहन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। खंडपीठ द्वारा पारित फैसले के आलोक में रिट याचिका में उठाये गये मुद्दे का निपटारा पहले ही हो चुका है।
एस.आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ (1994)
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के मामले में भारत के संवैधानिक न्यायशास्त्र (जुरिस्प्रूडेंस) में एक महत्वपूर्ण उदाहरण साबित होता है। केंद्र-राज्य संबंधों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे की जांच के कारण यह ऐतिहासिक निर्णय महत्वपूर्ण है। भारत संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था का पालन करता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करके, फैसले ने राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की बर्खास्तगी को प्रभावी ढंग से रोक दिया।
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी करने की शक्ति पूर्ण नहीं है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यह भी निष्कर्ष निकाला कि फ्लोर टेस्ट ने पुष्टि की कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है।
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) का विश्लेषण
उपर्युक्त मामले में फैसले ने अध्यादेशों से संबंधित न्यायिक समीक्षा के दायरे को व्यापक बना दिया और उनके निहितार्थों में पारदर्शिता भी बढ़ा दी। यह अदालत को राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के कार्यों की जांच करने का अधिकार देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी वैधता के गहन मूल्यांकन के माध्यम से अध्यादेश जारी करना आवश्यक समझा जाता है।
अक्सर हम सरकार को अध्यादेशों और उन्हें बार-बार जारी करने के माध्यम से विचार-विमर्श के संवैधानिक ढांचे को दरकिनार करते हुए देखते हैं। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) के मामले में फैसला ने अध्यादेशों के लिए न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ाया, जिससे इसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। यह निर्णय अदालत के प्राधिकार को राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की समीक्षा करने का अधिकार देता है।
संविधान का अनुच्छेद 123 एक असाधारण उपाय के रूप में अध्यादेश का उपयोग करने के नियमों की रूपरेखा देता है। यह स्पष्ट है कि सरकार इसका उपयोग नियमित कानून बनाने की तरह कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकारियों को संसद से अधिक शक्तिशाली बनाता है। अदालत का फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्यपालिका द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है। इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि अध्यादेश समाप्त होने के बाद भी कुछ अधिकार, विशेषाधिकार या दायित्व जारी रहने चाहिए या नहीं। हालांकि, समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ कोई अध्यादेश सार्वजनिक हित के विपरीत होने के बावजूद स्वाभाविक रूप से अपरिवर्तनीय होता है। भले ही यह फैसले में एक अंतर है, लेकिन यह समग्र रूप से फैसले को कमजोर नहीं करेगा।
चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का तर्क काफी हद तक डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986) फैसले पर आधारित था। जिसमें माना गया कि विधायी जांच के लिए रखे बिना अध्यादेशों को फिर से जारी करना स्पष्ट रूप से संवैधानिकता के मूल सार का उल्लंघन करता है और शीर्ष न्यायालय ने भी यह स्पष्ट रूप से माना था कि संसदीय सर्वोच्चता कार्यपालिका पर हावी रहेगी।

निष्कर्ष
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा पारित आदेश के प्रति एक महत्वपूर्ण संतुलन बनाता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कार्यपालिका को उन्हें दिए गए अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और यह भी उजागर किया कि यदि संसद काम नहीं कर रहा है तो अध्यादेश की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रख्यापित की जानी चाहिए।
निर्णय बहुमत की राय के साथ दिया गया था और यद्यपि अध्यादेश समाप्त होने के बाद हम अधिकारों और कर्तव्यों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसमें अभी भी एक अंतर है, लेकिन यह फैसले के रुख को कमजोर नहीं करता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले की व्याख्या खुली रहेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
अध्यादेशों के प्रख्यापन और पुनः प्रख्यापित से क्या तात्पर्य है?
अध्यादेश एक कानून है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा तब प्रख्यापित किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। इसका प्रभाव किसी भी कानून के समान है और तत्काल कार्रवाई करने में मदद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी सिफारिश की जानी चाहिए।
किसी अध्यादेश को दोबारा जारी करने का मतलब अध्यादेश की अवधि बढ़ाना है। आम तौर पर, कोई अध्यादेश सदनों की पुनः बैठक की तारीख से छह सप्ताह के बाद लागू होना बंद हो जाता है, लेकिन पुन: प्रख्यापित विधायी विचार-विमर्श के बाद ही वैध होता है और यदि ऐसा नहीं होता है, तो उक्त अध्यादेश को कानून की नजर में असंवैधानिक और अमान्य माना जाएगा।
किसी न्यायाधीश की सहमति और असहमति की राय का क्या मतलब है?
एक सहमतिपूर्ण राय एक न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की जाती है जो फैसले के बहुमत से सहमत होता है लेकिन विभिन्न कारणों या अतिरिक्त टिप्पणियों के लिए। यह वैकल्पिक या अतिरिक्त कानूनी तर्क भी प्रदान करता है जो बहुमत के निर्णयों का समर्थन करता है। यह पूरक कानूनी दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है लेकिन निर्णय में परिवर्तन नहीं करता है।
एक असहमति पूर्ण राय एक न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की जाती है जो न केवल किसी मामले में बहुमत के फैसले से असहमत है बल्कि बहुमत के कानूनी तर्क या निष्कर्षों से असहमति के साथ-साथ मामले पर एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करता है। हालांकि असहमति पूर्ण राय का मामले के नतीजे पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यह भविष्य के फैसले को प्रभावित कर सकता है और बहुमत द्वारा भरोसा किए गए मौजूदा उदाहरणों की आलोचना या अस्वीकार भी कर सकता है।
संदर्भ
- https://www.mondaq.com/india/constitutional–administrative-law/742420/re-promulgation-of-ordinance-is-a-fraud-on-the-constitution–analysis-in-light-of-krishna-kumar-singh-v-state-of-bihar
- https://www.livelaw.in/placing-ordinance-legislature-mandatory-re-promulgation-fraud-constitution-sc-7-judge-bench/
- https://www.scobserver.in/reports/krishna-kumar-singh-bihar-re-promulgation-of-ordinances-judgment-of-the-supreme-court-in-plain-english/
- https://main.sci.gov.in/jonew/judis/44452.pdf
- https://legaldesire.com/case-comment-on-krishna-kumar-singh-anr-v-state-of-bihar-ors/
- https://lawtimesjournal.in/krishna-kumar-singh-anr-vs-state-of-bihar-ors/
- https://legalvidhiya.com/krishna-kumar-singh-anr-v-state-of-bihar-ors-2017-3-scc-1/
- https://vidhinama.com/case-analysis-krishna-kumar-singh-anr-vs-state-of-bihar-ors-2017-3-supreme-court-cases-scc-1/#footnote_9_1995
- https://www.scobserver.in/wp-content/uploads/2021/10/13218.pdf
- https://www.scobserver.in/wp-content/uploads/2021/10/44452.pdf
- https://www.scobserver.in/wp-content/uploads/2021/10/208120.pdf
- https://www.casemine.com/judgement/in/5609ac19e4b014971140e06d







