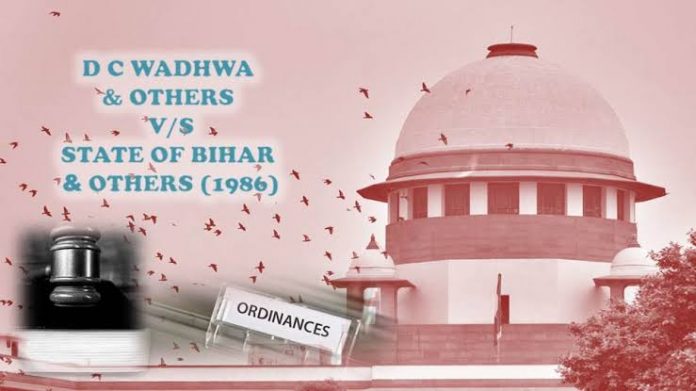यह लेख Bhuvan Malhotra द्वारा लिखा गया था और इसे Pruthvi Ramakanta Hedge द्वारा आगे अपडेट किया गया है। यह लेख अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) पर आधारित डॉ. डी.सी. वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1986) के मामले के तथ्यों, मुद्दों और निर्णय से संबंधित है। लेख में अध्यादेश का अवलोकन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति को भी शामिल किया गया है। इस लेख का अनुवाद Ayushi Shukla के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान एक नियम पुस्तिका की तरह होता है जिसका पालन सभी को करना होता है। यह तय करता है कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए और नागरिकों के पास क्या अधिकार हैं। भारत में भारतीय संविधान को ‘मातृ कानून’ माना जाता है। सरकार के अंग या शाखाएँ, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, क्रमशः को निर्णय लेते समय, कोई कानून बनाते समय और कोई निर्णय सुनाते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त कार्य भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार किए जाएँ।
आम तौर पर, कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह होता है जो उन कानूनों पर बहस करते हैं और मतदान करते हैं। हालाँकि, अध्यादेश नामक एक प्रावधान है जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सामान्य विधायी प्रक्रिया से गुजरे बिना कानून बनाने की अनुमति देता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है जिसे राज्यपाल या राष्ट्रपति तब जारी कर सकते हैं जब विधायिका सत्र (सेशन) में न हो। इसका उपयोग आपातकालीन या अत्यावश्यक स्थितियों में किया जाता है जब विधायिका की बैठक और कानून पारित करने के लिए प्रतीक्षा करना अव्यावहारिक होगा। हालाँकि, जब इन अध्यादेशों को बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक बार-बार जारी किया जाता है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? डॉ. डी.सी. वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1987) के मामले में भी इसी पर चर्चा की गई थी, जिसकी चर्चा इस लेख में और विस्तार से की जाएगी।
डॉ. डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1986) का विवरण
मामले का नाम
डॉ. डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
फैसले की तारीख
20 दिसंबर, 1986
सर्वोच्च न्यायालय पीठ
- भारत के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती
- माननीय न्यायमूर्ति के.एन. सिंह
- माननीय न्यायमूर्ति एम.एम.दत्त
- माननीय न्यायमूर्ति जी.एल.ओझा
- माननीय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा

मामले के पक्ष
याचिकाकर्ता
डॉ. डी.सी. वाधवा एवं अन्य
प्रतिवादी
बिहार राज्य एवं अन्य
समतुल्य उद्धरण (साईटेशंस)
एआईआर 1987 एससी 579, 1986/आईएनएससी/280, जेटी 1987 (1) एससी 70, 1986 (2) स्केल 1174, (1987) 1 एससीसी 378, [1987] 1 एससीआर 798
मामले का प्रकार
रिट याचिका संख्या 412-15/1984
किसके द्वारा प्रस्तुत
याचिकाकर्ता
अधिवक्ता अर्थात् सोली जे. सोराबजी, जे.बी. दादाचंजी, रविन्द्र नारायण, टी.एन. अंसारी और जोएल पेरेज।
प्रतिवादी
अधिवक्ता अर्थात् एल.एन. सिन्हा, जय नारायण, पी.पी. सिंह, डी. गोवर्धन और सुषमा रेलन।
निर्णय के लेखक
न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती
न्यायालय का नाम
माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय
संबंधित कानून
भारतीय संविधान, 1950 के अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 32
डॉ. डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1986) से संबंधित कानूनी पहलू
अध्यादेश
अर्थ
सामान्य तौर पर, अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल (यूनियन कैबिनेट) की सिफारिश के आधार पर जारी किया गया कानून होता है, जब संसद सत्र में नहीं होती है। इसी तरह, भारतीय राज्यों के राज्यपाल भी अध्यादेश पारित कर सकते हैं जब संबंधित विधान सभा (लेजिस्लेटिव एसेंबली) (या विधान सभा और विधान परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) दोनों, यदि यह द्विसदनीय विधायिका है) सत्र में नहीं होती है।
अध्यादेश का इतिहास
भारत में अध्यादेशों का इतिहास भारत सरकार अधिनियम, 1919 से शुरू हुआ। भले ही ‘अध्यादेश’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन इस अधिनियम ने सामान्य विधायी प्रक्रिया के बिना कानून बनाने की अनुमति दी, अगर राज्यपाल की परिषद उन्हें पारित नहीं करती। अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक उनके कर्तव्यों के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है, तो वे इसे कानून बना सकते हैं, भले ही परिषद असहमत हो। इसने अध्यादेशों के लिए मंच तैयार किया, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अस्थायी कानून हैं जब विधायिका सत्र में नहीं होती है। वे तब से भारत की कानूनी प्रणाली में आम हो गए हैं, लेकिन कुछ नियमों और सीमाओं के अधीन हैं।
धारा 13 में एक प्रावधान है जो विधेयक को कानून बनाने की अनुमति देता है, भले ही वह विधान परिषद द्वारा पारित न किया गया हो। यह प्रावधान तब लागू होता है जब राज्यपाल की विधान परिषद विधेयक पेश करने से इनकार कर देती है या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित प्रारूप में इसे पारित करने में विफल रहती है। ऐसे मामलों में, राज्यपाल यह प्रमाणित कर सकते हैं कि विषय वस्तु के संबंध में उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विधेयक का पारित होना आवश्यक है।
परिणामस्वरूप, भले ही परिषद सहमत न हो, विधेयक को पारित माना जाएगा। फिर, राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ, यह कानून बन सकता है। यह कानून या तो बिल्कुल वैसा ही हो सकता है जैसा इसे पहली बार पेश किया गया था या फिर परिषद के विचार के लिए सुझाए गए संस्करण में हो सकता है। यह प्रावधान विधायी प्रक्रिया के सामान्य चरणों से गुजरे बिना कानून बनाने की अनुमति देता है।
राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल की उस शक्ति से संबंधित है जिसके तहत वह राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश नामक कानून बना सकता है। अनुच्छेद 213 में कहा गया है कि:
- यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य विधान सभा (या विधान परिषद होने पर दोनों सदन) के सत्र में न होने पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
- यदि किसी समान कानून के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो, या यदि राज्यपाल सामान्यतः ऐसे कानून को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजता हो, या यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई समान कानून अवैध हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।
- अध्यादेशों में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों के समान ही शक्ति होती है, लेकिन उन्हें विधान सभा (या दोनों सदनों) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और विधानमंडल द्वारा अनुमोदित न किए जाने पर छह सप्ताह के बाद समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को रद्द भी कर सकते हैं।
- अगर अध्यादेश में कुछ ऐसा शामिल है जिसकी अनुमति विधानमंडल द्वारा पारित नियमित कानून में नहीं होगी, तो अध्यादेश का वह हिस्सा अमान्य हो जाता है। हालाँकि, अगर राष्ट्रपति ने राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का निर्देश दिया है, तो इसे विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है।

शक्ति का पृथक्करण (सेप्रेशन)
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सरकार की एक आधारभूत संरचना है, जहाँ अधिकार कई शाखाओं के बीच वितरित किए जाते है। आम तौर पर, लोकतांत्रिक देशों में, ये शाखाएँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती हैं। यह सिद्धांत मानता है कि एक स्वतंत्र लोकतंत्र में, प्रत्येक शाखा की स्पष्ट और अलग-अलग भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए। वे विवादों को रोकने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यह सुनिश्चित करके कि एक शाखा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इसका मतलब है कि कार्यपालिका को विधायी या न्यायिक कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए, विधायिका को कार्यकारी या न्यायिक कार्य नहीं करने चाहिए, और न्यायपालिका को विधायी या कार्यकारी कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। यह पृथक्करण शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और किसी एक शाखा को बहुत अधिक प्रभावशाली बनने से रोकती है।
डॉ. डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1986) के तथ्य
बिहार में एक आम प्रथा थी जिसमें सरकार विधानमंडल के माध्यम से उन्हें स्थायी कानून में बदले बिना बार-बार अध्यादेश जारी करती थी। राज्य विधानमंडल का सत्र समाप्त होने के बाद, उन्हीं अध्यादेशों को उसी विषय-वस्तु के साथ फिर से पेश किया जाता था। इस प्रथा के लिए जिन तीन विशिष्ट अध्यादेशों को चुनौती दी गई, वे हैं:
- बिहार वनोपज (फॉरेस्ट प्रोड्यूस) (व्यापार विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1983 – इस अध्यादेश ने बिहार में वनोपज के व्यापार को विनियमित किया। इसमें वनोपजों को कैसे खरीदा, बेचा या परिवहन किया जा सकता है, इसके बारे में नियम थे।
- बिहार मध्यवर्ती (इंटरमीडिएट) शिक्षा परिषद तृतीय अध्यादेश, 1983 – यह अध्यादेश बिहार मध्यवर्ती शिक्षा परिषद से संबंधित है। इसमें बिहार में मध्यवर्ती शिक्षा के संचालन या प्रबंधन के संबंध में प्रावधान हैं।
- बिहार ईंट आपूर्ति (नियंत्रण) तृतीय अध्यादेश, 1983 – यह अध्यादेश बिहार में ईंट आपूर्ति के नियंत्रण से संबंधित था। इसमें राज्य के भीतर ईंटों के निर्माण, वितरण या बिक्री के तरीके पर नियमन शामिल थे।
इन तीनों अध्यादेशों को बार-बार फिर से पेश किया गया। हालाँकि, अध्यादेशों को स्थायी कानून में बदले बिना फिर से पेश किया गया, जिससे इन अध्यादेशों की वैधता पर सवाल उठने लगे।
इस मामले में याचिकाकर्ता (1), डॉ. डी.सी. वाधवा पुणे में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और उन्होंने बिहार के राज्यपाल द्वारा विभिन्न अध्यादेशों को फिर से जारी करने की राज्यपाल की सामान्य शक्ति को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बिहार के राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति के दुरुपयोग के बारे में व्यापक शोध और प्रकाशन किया था क्योंकि बिहार सरकार ने 1967 और 1981 के बीच 256 अध्यादेश जारी किए थे और इन 256 अध्यादेशों को अध्यादेश की किसी भी सामग्री को बदले बिना या इसे अधिनियम में बदलने की कोशिश किए बिना फिर से जारी करके एक से चौदह साल की अवधि के लिए जीवित रखा गया था।
याचिकाकर्ता (2, 3 और 4) ऐसे व्यक्ति थे जो ऊपर उल्लिखित अध्यादेशों के प्रावधानों से सीधे प्रभावित हुए थे। याचिकाकर्ता संख्या 2 एक किसान था जो अनिगारा नामक गांव में अपनी जमीन पर वन उपज उगाता था। वह बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) तृतीय अध्यादेश, 1983 के खंड (5) से प्रभावित था। इस अध्यादेश ने कुछ वन उपज की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया और उनकी बिक्री के लिए राज्य का एकाधिकार बना दिया। इस अध्यादेश के खंड (7) ने सरकार को वह मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी जिस पर वह या अधिकृत अधिकारी याचिकाकर्ता संख्या 2 जैसे उत्पादकों से वन उपज खरीद सकते थे। इन प्रावधानों ने उसकी अपनी उपज को स्वतंत्र रूप से बेचने की क्षमता को सीमित कर दिया, इसलिए वह अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने में रुचि रखता था।
याचिकाकर्ता संख्या 3 पटना के एएन कॉलेज में मध्यवर्ती (विज्ञान) कक्षा में पढ़ने वाला छात्र था, जो बिहार मध्यवर्ती शिक्षा परिषद तीसरे अध्यादेश से प्रभावित था, जो उनकी शिक्षा के पहलुओं को विनियमित करता था। हालांकि इस अध्यादेश की बारीकियों पर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यह स्पष्ट था कि इसने याचिकाकर्ता संख्या 3 के अधिकारों को प्रभावित किया है या संभावित रूप से प्रभावित कर सकता है, इस प्रकार इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई।
इसी तरह, याचिकाकर्ता संख्या 4 पटना में साउथ बिहार एजेंसी नामक ईंट निर्माण व्यवसाय के मालिक थे। वे बिहार ईंट आपूर्ति (नियंत्रण) तृतीय अध्यादेश से प्रभावित थे, जिसने राज्य सरकार को ईंट निर्माण और बिक्री के विभिन्न पहलुओं, जिसमें कीमतें भी शामिल हैं, पर नियंत्रण दिया था। इन प्रावधानों ने याचिकाकर्ता के व्यवसाय को प्रभावित किया, इसलिए उन्होंने इस अध्यादेश की संवैधानिकता को भी चुनौती दी।
रिट याचिकाओं की कार्यवाही के दौरान, विधानमंडल द्वारा उल्लिखित अध्यादेशों में से दो के प्रावधानों को कानून में बदल दिया गया। हालाँकि, तीसरा अध्यादेश, यानी बिहार मध्यवर्ती शिक्षा परिषद तीसरा अध्यादेश, 1983 अभी भी लागू था। इसके प्रावधानों को शामिल करने वाला एक विधेयक राज्य विधानमंडल के समक्ष विचाराधीन था, जिसे आगे के मूल्यांकन के लिए चुनाव समिति को भेजा गया था।
राज्यपाल की अध्यादेश को फिर से जारी करने की सामान्य शक्ति की न्यायालय द्वारा जांच की गई क्योंकि कई अध्यादेशों को तीस से अधिक बार फिर से जारी किया गया था। तत्काल चुनौती उन तीन अध्यादेशों को लेकर थी जिन्हें 10-14 वर्षों की अवधि तक जीवित रखा गया था।
मामले के मुद्दे
मुख्य मुद्दा यह था कि क्या राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए अध्यादेश को यंत्रवत् (मेकेनिकली) फिर से जारी कर सकते हैं, और इस प्रकार अनुच्छेद 213 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति (विधानमंडल से) ले सकते हैं।
इस मामले में मुद्दा संवैधानिक कानून के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्यपालिका अध्यादेशों को फिर से जारी करके कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में ले रही थी। कार्यपालिका का यह व्यवहार संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है क्योंकि प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों यानी विधायिका द्वारा शासित होने का अधिकार है, न कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए उप-कानूनों द्वारा।
दिए गये तर्क
प्रतिवादी
प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने रिट याचिकाओं के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि:
- याचिकाकर्ताओं को ये रिट याचिकाएं लाने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि दो अध्यादेश पहले ही संसद के अधिनियम में अधिनियमित किए जा चुके थे और तीसरे अध्यादेश को अधिनियम में अधिनियमित करने के प्रस्ताव के रूप में भेजा गया था, इस प्रकार यह प्रश्न केवल शैक्षणिक प्रकृति का था।
- याचिकाकर्ता, जो मुख्यतः बाहरी लोग हैं, को सरकार के अध्यादेशों को फिर से जारी करने की प्रथा को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
- न्यायालय में उठाया गया मुद्दा केवल सैद्धांतिक (थियोरिटिकल) है और इस पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए।
- अदालत को यह जांच नहीं करनी चाहिए कि राज्यपाल ने अध्यादेश जारी करने से पहले आवश्यक शर्तों का पालन किया था या नहीं।
प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न तर्क दिए गए कि याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका जारी रखने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे बाहरी व्यक्ति थे, जिनका अध्यादेशों के फिर से जारी करने की वैधता को चुनौती देने में कोई कानूनी हित नहीं था।

याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि एक नागरिक के तौर पर उसे संविधान के अनुसार चलने वाले कानूनों से शासित होने पर जोर देने का अधिकार है, न कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके कार्यकारी शाखा द्वारा बनाए गए कानूनों से। जबकि उसे किसी विशिष्ट अध्यादेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह सीधे उसे प्रभावित न करे, उन्हें बिहार में विधायिका द्वारा कानूनों में बदले बिना बार-बार अध्यादेश जारी करने की व्यापक प्रथा को चुनौती देने का अधिकार है। यह स्पष्ट रूप से जनहित की रक्षा के लिए है”, और इसलिए, याचिकाकर्ता को अपनी रिट याचिकाओं को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
हालाँकि, इन दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने रिट याचिकाओं को अनुमति देने का फैसला किया।
डॉ. डी.सी. वाधवा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1986) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा विधानमंडल से मंजूरी लिए बिना बार-बार अध्यादेश जारी करना संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन है। इसके अलावा, न्यायालय ने अपने निर्णय के समर्थन में पिछले मामलों में लिए गए न्यायिक निर्णयों पर भी गौर किया।
उन्होंने के.सी. गजपति नारायण देव एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य (1953) के मामले से एक नियम की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार वास्तव में क्या कर रही है, न कि केवल इस बात पर कि वे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने अध्यादेश शक्तियों का प्रयोग करने में राष्ट्रपति और राज्यपाल के आचरण के बीच तुलना की। समान अधिकार रखने के बावजूद, न्यायालय ने पाया कि राष्ट्रपति ने अध्यादेशों की समाप्ति के बाद उन्हें फिर से जारी करने की वही प्रथा नहीं है। पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष डिप्टी कलेक्टर, मद्रास एवं अन्य (1964) के मामले से ली गई यह टिप्पणी राज्यपाल के कार्यों की अनियमितता और अनुचितता को रेखांकित करती है।
इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपातकालीन शक्ति की तरह है, जिसका उद्देश्य ऐसी स्थितियों के लिए है जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि राज्यपाल के पास यह शक्ति तो है, लेकिन कानून बनाने का मुख्य अधिकार विधानमंडल के पास है, कार्यपालिका के पास नहीं। अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति विधानमंडल के फिर से शुरू होने तक तत्काल स्थितियों को संबोधित करने के लिए एक अस्थायी उपाय है। अध्यादेशों की अवधि सीमित होनी चाहिए और उनका उपयोग विधानमंडल के कानून बनाने के कार्य को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
निर्णय का आलोचनात्मक विश्लेषण
इन सभी दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया क्योंकि तीसरा अध्यादेश, हालांकि संसद के समक्ष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, अभी भी लागू था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल मनमाने ढंग से नए नियम नहीं बना सकते। वे केवल आपात स्थितियों के लिए अस्थायी नियम बना सकते हैं, और विधानमंडल के दोबारा बैठने पर ये नियम वैध नहीं रह जाते।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वर्तमान में प्रभावी बिहार मध्यवर्ती शिक्षा परिषद अध्यादेश, 1983 को असंवैधानिक घोषित किया गया है और इसलिए यह अमान्य है। यह कानून कानूनी रूप से वैध या बाध्यकारी नहीं है क्योंकि यह भारत के संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसलिए, इस अध्यादेश के आधार पर किए गए किसी भी कार्य या विनियमन को कानूनी रूप से अमान्य माना जाता है।
न्यायालय ने आगे कहा कि राज्यपाल का यह कार्य असंवैधानिक है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित राज्यपाल के अधिकार से परे है। न्यायालय ने आगे कहा कि बिहार में कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं का पालन किए बिना लंबे समय तक कानून बनाकर विधायिका की तरह काम कर रही है। यह व्यवहार अनुचित और संवैधानिक ढांचे के खिलाफ माना जाता है।
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लंबे समय तक अध्यादेशों पर निर्भर रहने के बजाय, सरकार को उन प्रावधानों को कानून बनाने के लिए विधायिका में विधेयक पेश करके उचित विधायी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि देश में अध्यादेश-राज की प्रथा नहीं होनी चाहिए; यह कह रहा है कि कार्यपालिका को अध्यादेशों के माध्यम से लंबे समय तक कानून बनाकर अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और इसके बजाय कानून बनाने की प्रक्रिया में विधायिका को शामिल करके संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करना चाहिए।
न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुसार कानून के शासन के महत्व पर भी जोर दिया। इसमें कहा गया है कि सरकार की सभी शाखाओं, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और कोई भी अन्य प्राधिकरण, को संवैधानिक सीमाओं के दायरे में काम करना चाहिए। यदि सरकार की कोई भी शाखा, विशेष रूप से कार्यपालिका, ऐसी प्रथाओं में संलग्न है जो इन संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती हैं, तो जनता के किसी भी सदस्य (जिसे याचिकाकर्ता संख्या 1 कहा जाता है) को रिट याचिका दायर करके ऐसी प्रथाओं को चुनौती देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, यह रेखांकित किया गया है कि ऐसी याचिकाओं की वैधता पर विचार करना और उस पर निर्णय देना सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है।
अध्यादेश जारी करना राज्यपाल द्वारा पुष्टि की गई एक विशेष शक्ति है। इसका उद्देश्य बड़ी समस्याओं से जल्दी निपटना है। लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल अस्थायी नियम बना सकते हैं जिन्हें अध्यादेश कहा जाता है जब कोई आपात स्थिति होती है और नियमित कानून बनाने वाली संस्था, विधायिका, सत्र में नहीं बैठती है। भले ही विधायिका आमतौर पर कानून बनाती है, लेकिन आपात स्थिति में राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं। हालाँकि, हर अध्यादेश को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और यह विधायिका के फिर से बैठने के बाद केवल छह सप्ताह तक रहता है जब तक कि विधायिका इस तरह के अध्यादेश को लागू करके इसे लंबे समय तक रखने के लिए सहमत न हो। इस तरह, अध्यादेशों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर और सीमित समय के लिए किया जाता है। अध्यादेशों को केवल थोड़े समय के लिए, आमतौर पर छह सप्ताह तक, नियमित सांसदों को उचित कानून बनाने का मौका देने के लिए चलना चाहिए। यदि वे उस समय के भीतर ऐसा नहीं करते हैं, तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। सरकार विधायिका की स्वीकृति के बिना उसी अध्यादेश को फिर से जारी नहीं कर सकती। जब राज्यपाल द्वारा किसी आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है, तो विधायिका के फिर से मिलने के छह सप्ताह बाद यह अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि सरकार उन नियमों को उस समयावधि के बाद भी लागू रखना चाहती है, तो उसे विधानमंडल की मंजूरी लेनी होगी।
इस मुद्दे पर न्यायालय द्वारा निर्णय लेने का एक और कारण यह था कि न्यायालय ने पाया कि अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेशों को इस मुकदमे के लंबित रहने तक कभी भी फिर से जारी नहीं किया गया था, लेकिन बिहार सरकार विभिन्न अध्यादेशों को जारी रखे हुए थी, जबकि परिपत्रों में स्पष्ट रूप से विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि अध्यादेशों के समाप्त होते ही उन्हें यंत्रवत् फिर से जारी कर दिया जाए। किसी अध्यादेश को अधिकतम 39 बार फिर से जारी किया गया।
अंत में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका के पास जाए बिना एक से चौदह वर्ष की अवधि के लिए अध्यादेशों को यांत्रिक रूप से फिर से जारी करना कार्यपालिका द्वारा शक्ति का एक रंग-रूपी प्रयोग था और उसने निर्णय दिया कि अध्यादेशों को फिर से जारी करना असंवैधानिक था। राज्यपाल द्वारा विधायिका की अनदेखी करना और उसी अध्यादेश को बार-बार जारी करना गलत होगा क्योंकि इससे उन्हें बहुत अधिक शक्ति मिल जाएगी और यह संविधान के प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल की शक्ति का उल्लंघन करता है। न्यायालय की भूमिका के बारे में, वे यह सवाल नहीं कर सकते कि अध्यादेश जारी करते समय राज्यपाल संतुष्ट थे या नहीं। लेकिन, इस मामले में, मुद्दा राज्यपाल की संतुष्टि के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि क्या राज्यपाल के पास विधायिका को शामिल किए बिना उसी अध्यादेश को बार-बार जारी करने की शक्ति है। इसका उत्तर है नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति भगवती द्वारा दिया गया निर्णय तब विफल हो जाता है जब न्यायालय कहता है कि ऐसे समय आ सकते हैं जब संसद समय की कमी के कारण प्रख्यापित अध्यादेशों पर विचार नहीं कर सकती।

निर्णय से जुड़ी समस्याएं
बेशक, यह कई कारणों से एक दोषपूर्ण निर्णय था। सबसे पहले, इसका एक कारण यह है कि न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि इन असफल अध्यादेशों द्वारा किए गए प्रभावों का क्या होगा। इस मामले और टी. वेंकट रेड्डी के मामले में सामंजस्य स्थापित करने का अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि ऐसे असफल अध्यादेशों के प्रभाव जो फिर से जारी किए जाते हैं, वैसे ही बने रहेंगे, यद्यपि फिर से जारी अध्यादेशों को असंवैधानिक प्रकृति का घोषित किया गया है। इसके अलावा, इस मामले और टी. वेंकट रेड्डी के मामले के बीच न्यायिक समीक्षा के दायरे में एक गलत अंतर है। एक अन्य प्रतिकूल प्रभाव मामले में दिए गए समस्याग्रस्त अपवादों के कारण था क्योंकि निर्णय के बाद अध्यादेशों के फिर से जारी करने में वृद्धि हुई; 1991 और 1993 के बीच 53 अध्यादेश फिर से जारी किए गए और कुछ को कम से कम पांच बार प्रख्यापित किया गया।
इस मामले का बाद में कृष्ण कुमार बनाम बिहार राज्य (2017) के मामले में भी हवाला दिया गया, जिसमें अध्यादेशों के फिर से जारी करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया था और फिर से जारी करना भी कुछ ऐसा था जिस पर न्यायालय ने टिप्पणी की थी। इस मामले में अदालत ने डी.सी. वाधवा के मामले में रखे गए दृष्टिकोण से थोड़ा अलग रुख अपनाया और कहा कि अध्यादेश का फिर से जारी करना एक असंवैधानिक प्रथा है; आवश्यक बहस के लिए अध्यादेश को अनिवार्य रूप से संसद में रखा जाना चाहिए और ऐसा नहीं करना संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अंतर केवल डी.सी. वाधवा मामले में दिए गए अपवादों का था, लेकिन न्यायमूर्ति लोकुर की राय से यह पता चलता है कि अदालत ने डी.सी. वाधवा मामले को स्पष्ट रूप से खारिज नहीं किया, बल्कि उससे केवल मतभेद व्यक्त किया। इसलिए ऐसा लगता है कि कृष्ण कुमार के मामले ने फिर से जारी करने की प्रथा का उत्तर अधूरा छोड़ दिया है।
कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य का विश्लेषण (2017)
उपर्युक्त मामले के निर्णय ने अध्यादेशों से संबंधित न्यायिक समीक्षा के दायरे को व्यापक बनाया और उनके प्रभावों में पारदर्शिता को भी बढ़ाया। यह न्यायालय को राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के कार्यों की जांच करने का अधिकार देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक अध्यादेश जारी करना इसकी वैधता के गहन मूल्यांकन के माध्यम से आवश्यक समझा जाता है।
अक्सर हम सरकार को अध्यादेशों के माध्यम से विचार-विमर्श के एक संवैधानिक ढांचे को पारित करते हुए और उनकी बार-बार फिर से जारी करते हुए देखते हैं। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) के मामले में फैसले ने अध्यादेशों के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे को व्यापक बना दिया, जिससे इसकी पारदर्शिता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई। फैसला न्यायालय को अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति की समीक्षा करने का अधिकार देता है।
संविधान का अनुच्छेद 123 एक असाधारण उपाय के रूप में अध्यादेश का उपयोग करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। यह स्पष्ट है कि सरकार इसका उपयोग नियमित कानून बनाने की तरह कर रही है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में अधिकारियों को संसद की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाती है। अदालत का फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्यपालिका द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की जांच करता है। इसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि अध्यादेश की अवधि समाप्त होने के बाद कुछ अधिकार, विशेषाधिकार या दायित्व जारी रहने चाहिए या नहीं। हालाँकि, समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक अध्यादेश जनहित के विपरीत होने के बावजूद स्वाभाविक रूप से अपरिवर्तनीय होता है। भले ही यह निर्णय में एक अंतर है, लेकिन यह समग्र रूप से निर्णय को कमजोर नहीं करेगा।
चूंकि सर्वोच्च न्यायालय का तर्क काफी हद तक डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1986) के फैसले पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि विधायी जांच के लिए रखे बिना अध्यादेशों को फिर से जारी करना स्पष्ट रूप से संवैधानिकता के मौलिक सार का उल्लंघन करता है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी बहुत स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि संसदीय सर्वोच्चता कार्यपालिका पर प्रबल होगी।
क्या इस फैसले को बेहतर तरीके से निपटाया जा सकता था?
डी.सी. वाधवा के फैसले को बेहतर तरीके से कैसे निपटाया जा सकता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें संविधान के मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने वाली सभा के सदस्यों की मंशा को देखना होगा, संविधान में ऐसे अनुच्छेदों को शामिल करने और मसौदा तैयार करने के समय दिए गए तर्कों की जांच करनी होगी, कि वे हमें इन अनुच्छेदों के बारे में क्या समझाना चाहते थे। इसके बाद हम कुछ अन्य अधिकार क्षेत्रों को देख सकते हैं, जहां अनुच्छेद 123 और 213 में परिकल्पित ऐसी शक्ति मौजूद है और ये देश अध्यादेशों के फिर से जारी करने की प्रथा को कैसे देखते हैं।
संविधान सभा की बहस
राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति औपनिवेशिक (कोलोनियल) अतीत की विरासत है और अंग्रेजों ने कानून बनाने की इस शक्ति को खत्म करने का फैसला किया लेकिन मसौदा समिति ने उन्हें संविधान में अनुच्छेद 123 और 213 के रूप में शामिल किया। इन्हें भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 42 और 43 से अपनाया गया था, जिसने भारत के गवर्नर-जनरल को समानांतर विधायी शक्ति प्रदान की थी। संविधान सभा की बहसों में इन अनुच्छेदों की कड़ी आलोचना की गई क्योंकि वे निर्वाचित और प्रतिनिधि राजनीति के अनुकूल नहीं थे।
संविधान में प्रावधान है कि अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः सत्र के छह सप्ताह के भीतर सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अध्यादेश के लागू होने की अधिकतम अवधि लगभग साढ़े सात महीने होगी। बहसों में अध्यादेश की अवधि की बहुत आलोचना की गई, जैसे एच.वी. कामथ को लगा कि पुनः सत्र की तिथि से छह सप्ताह का समय बहुत लंबा है और उन्हें चिंता थी कि तानाशाही के लिए इच्छुक राष्ट्रपति अनुच्छेदों का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। एच.एन. कुन्जू भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, उन्होंने छह सप्ताह के बजाय चार सप्ताह की वकालत की। हालांकि, अध्यादेश के खिलाफ सबसे मुखर आवाज के.टी. शाह की थी, जिन्होंने अध्यादेश को ऐसी असाधारण परिस्थितियों से एक मिनट भी अधिक समय तक न चलने देने की वकालत की और संसद के पुनः सत्र के तुरंत बाद अध्यादेश को समाप्त करने का सुझाव दिया। सदस्यों ने अध्यादेश बनाने की शक्ति के विचार के खिलाफ शायद ही कुछ कहा, लेकिन चर्चा अध्यादेश की प्रकृति और दायरे तथा अध्यादेश पर वे क्या सीमाएं लगा सकते हैं, तक ही सीमित थी। अंबेडकर ने इन सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया और अनुच्छेदों को आज के रूप में शामिल कर लिया गया। शुभंकर दाम के अनुसार, अंबेडकर आने वाले राष्ट्रपतियों पर बहुत अधिक भरोसा करते थे और अंबेडकर का मानना था कि चूंकि इन अनुच्छेदों में कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्ति दी गई है, इसलिए उत्तराधिकारी संविधान के इन प्रावधानों का उपयोग करने में बहुत सावधान और अत्यंत सतर्क होंगे और उन्हें यह भी भरोसा था कि इन प्रावधानों का उपयोग केवल गंभीर आपातकाल की स्थिति में ही किया जाएगा और कार्यपालिका अध्यादेश को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहने देगी। साथ ही, संविधान सभा ने अध्यादेश बनाने की शक्ति पर एक ठोस सीमा के विचार को अस्वीकार कर दिया।

क्या किया जा सकता था?
सबसे पहले, यदि न्यायालय स्वयं फिर से जारी करने की प्रथा को असंवैधानिक कह रहा है, तो न्यायमूर्ति भगवती द्वारा दिए गए अपवादों की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय यह कहने के बजाय कि अध्यादेश से निपटने के लिए विधायकों के लिए सत्र बहुत छोटा हो सकता है, इसके बजाय अध्यादेश से निपटने के लिए सत्र की अवधि बढ़ाने का सुझाव दे सकता था क्योंकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसी आकस्मिक स्थिति के उत्पन्न होने पर निर्भर करती है। यदि विधायक उस आकस्मिक स्थिति से नहीं निपट रहे हैं, तो इसका अर्थ यह होगा कि या तो विधायक ऐसी समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं या समस्या अपने आप में इतनी आकस्मिक नहीं थी और इसे फिर से शुरू करने के लिए अगले सत्र का इंतजार किया जा सकता था।
दूसरी बात जो न्यायालय को सुनिश्चित करनी चाहिए थी, वह यह है कि पहले से ही समाप्त हो चुके या व्यतीत हो चुके अध्यादेश से पर्याप्त समानता रखने वाले किसी भी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं किया जाना चाहिए। यह वर्षों की संख्या और अध्यादेश को फिर से प्रख्यापित किए जाने की संख्या को देखते हुए आवश्यक हो जाता है। एक उदाहरण से समझाने के लिए, मान लीजिए कि राज्य किसी आपराधिक गतिविधि के लिए अधिकतम 14 वर्षों की सज़ा देने वाला अध्यादेश लेकर आता है और वह संसद के सामने ऐसे अध्यादेश को अधिनियमित करने का प्रस्ताव नहीं करता है, बल्कि इसके समाप्त हो जाने के बाद राज्य एक नया अध्यादेश प्रख्यापित करता है जो उसी गतिविधि के लिए 12 वर्षों की सज़ा देता है।
दोनों अध्यादेशों को देखते हुए राज्य आसानी से यह तर्क दे सकता है कि दोनों अध्यादेश अलग-अलग हैं क्योंकि सजा की अवधि कम कर दी गई है, इसलिए यह समाप्त हो चुके अध्यादेश का फिर से जारी करना नहीं है, लेकिन यह देखते हुए कि अध्यादेश द्वारा दंडित गतिविधि समान है, अध्यादेश को फिर से प्रचार के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायालय इस बात पर भी टिप्पणी करने में विफल रहा कि ऐसे अध्यादेशों द्वारा आए हुए प्रभावों का क्या होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फिर से जारी किए गए अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित किया गया है, न्यायालय ने यह निर्णय दिया होगा कि अध्यादेश का प्रभाव शुरू से ही शून्य हो जाएगा यदि इसे वापस ले लिया जाता है, या यह समाप्त हो जाता है।
सुझाव
जैसा कि ऊपर दिए गए तर्कों से पता चलता है, इन बहसों में टकराव का मुख्य मुद्दा वह समय अवधि थी जिसके लिए अध्यादेश प्रभावी रहेगा। संसद के पुनः एकत्र होने के बाद समय अवधि को कम करने का इरादा दिखाता है कि मसौदा तैयार करने वाले नहीं चाहते थे कि लोग कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों से शासित हों जो लंबे समय तक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अध्यादेश के फिर से जारी करने के बारे में कोई बहस नहीं हुई, जो स्पष्ट है क्योंकि फिर से जारी करने की प्रक्रिया कुछ और नहीं कर रही है, बल्कि विधायिका को आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अधिक समय दे रही है।
लेकिन प्रश्न इस दृष्टि से अधिक जटिल हो जाता है कि यदि उत्पन्न स्थिति वास्तव में इतनी आकस्मिक थी कि विधायक राज्य विधानसभा या संसद के अगले सत्र के आरंभ होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, तो क्या सत्र का पहला कार्य स्थिति से निपटना और प्रख्यापित अध्यादेश को संसद के अधिनियम के रूप में पारित कराना नहीं होता, क्योंकि अध्यादेश प्रख्यापित करना उत्पन्न स्थिति का एक अस्थायी समाधान मात्र है, क्योंकि वह अभी भी संसद का अधिनियम नहीं बन पाया है।
ब्राजील जैसे देश के संविधान में भी ऐसा प्रावधान मौजूद है, जहां कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है और संविधान कार्यपालिका को एक बार अध्यादेश समाप्त होने के बाद उसे फिर से जारी करने की भी अनुमति देता है; दूसरी बार अध्यादेश समाप्त होने के बाद अध्यादेश स्वतः ही कानून में परिवर्तित हो जाएगा। ब्राजील में अनुच्छेद के निर्माण के संदर्भ में एकमात्र अंतर यह है कि इसमें इस शक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं, जहां कार्यपालिका कोई अध्यादेश नहीं बना सकती। जैसा कि ऊपर के परिच्छेद (पैराग्राफ) में स्थापित किया गया है कि मसौदा समिति के सदस्यों का इरादा अध्यादेश बनाने की शक्ति के दायरे को सीमित करना नहीं था, ब्राजील के मॉडल के साथ जाना संभव नहीं होगा क्योंकि भारत में कार्यपालिका के पास ऐसी शक्ति का दायरा बहुत व्यापक है।

निष्कर्ष
अध्यादेश बनाने की शक्ति की कई लोगों ने कड़ी आलोचना की है और राजीव धवन जैसे लोग इस शक्ति को लोकतंत्र को धोखा देकर कानून बनाने के रूप में वर्णित करते हैं; इस तरह के अध्यादेश को फिर से जारी करना और भी बड़ा धोखा है क्योंकि यह एक ऐसी प्रथा (अध्यादेश बनाने) की निरंतरता है जो हमारे संविधान में परिकल्पित निर्वाचित और प्रतिनिधि राजनीति के साथ ठीक नहीं है। इसलिए, डी.सी. वाधवा के मामले में अदालत द्वारा इस प्रथा को स्वयं ही रोक दिया जाना चाहिए था या कृष्ण कुमार के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले को ख़ारिज कर देना चाहिए था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
डॉ. डी.सी. वाधवा मामले में मुख्य रूप से किस कानूनी सिद्धांत को चुनौती दी गई थी?
डॉ. डी.सी. वाधवा के मामले में प्राथमिक कानूनी चुनौती “अध्यादेश राज” की प्रथा के विरुद्ध थी, जहां राज्यपाल द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली कार्यपालिका, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, विधायिका की मंजूरी के बिना बार-बार एक ही अध्यादेश जारी करती थी।
क्या इस मामले के बाद भी कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है?
हां, कार्यपालिका (राष्ट्रपति या राज्यपाल) के पास अभी भी कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जब तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो और विधायिका सत्र में न हो। हालांकि, इस शक्ति का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए और यह नियमित विधायी प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता है, जैसा कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है।
इस मामले के संदर्भ में ‘लोकस स्टैंडी’ शब्द का क्या अर्थ है?
डॉ. डी.सी. वाधवा मामले के संदर्भ में, ‘लोकस स्टैंडी’ का अर्थ है किसी व्यक्ति का न्यायालय में कार्रवाई करने का अधिकार। यह मामला इस अवधारणा को पुष्ट करता है कि व्यक्ति अध्यादेशों की संवैधानिकता को न केवल तब चुनौती दे सकता है जब वे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हों, बल्कि तब भी जब वे संवैधानिक मूल्यों और शासन सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए जनहित में कार्य कर रहे हों।
संदर्भ