यह लेख Sangeet Kumar Khamari द्वारा लिखा गया है और इसे Titas Biswas द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया है। लेखक भारत में हिंदू कानून, इसकी उत्पत्ति, स्रोतों और प्रकृति को स्पष्ट करके इसकी बारीकियों पर प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा, लेखकों ने विधायी अधिनियमों और संप्रदायों (स्कूल) को स्पष्ट किया है जो हिंदू कानून के तहत शासन का गठन करते हैं। यह लेख भारत में हिंदू कानून के दायरे का दौरा प्रदान करता है, जहां इसने भारत के संविधान में भी अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
आरंभ करने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदू कानून रीति-रिवाजों और प्रथाओं, परंपराओं, विश्वासों और आधुनिक विधायी संरचना का व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) है। हिंदू कानून के तहत मुख्य अध्ययन धर्मशास्त्र की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमता है। धर्म की अवधारणा ने राजतंत्र की प्रथा को भी समाप्त कर दिया और कानून को राजा के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया। वैदिक काल लगभग 4,000 से 1000 ईसा पूर्व का है, जिसके परिणामस्वरूप यह 6,000 वर्ष पुराना है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किए गए हालिया शोध से यह पता लगाने में मदद मिली कि यह काल लगभग 8,000 वर्ष पुराना है। वेदों के साथ इसके संबंध और आज की तारीख में उनके अनुप्रयोग को देखते हुए, हिंदू कानून को उसी युग का माना जाता है। हिंदू कानून की संरचना हिंदू दर्शन और धार्मिक मान्यताओं में अच्छी तरह से निहित है, और सिद्धांत आधुनिक हिंदू कानून और इसकी शाखाओं में भी परिलक्षित होते हैं। इस विश्व की जनसंख्या 8 अरब है, जिसमें से 1.38 अरब लोग वर्तमान में भारत में रहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ धार्मिक मान्यताएँ विविध प्रकार की हैं। भारतीय कानूनी प्रणाली निम्नलिखित प्रकार के कानूनों का पालन करती है:
सामान्य कानून
ऐसे कानून जो व्यक्तियों के किसी विशिष्ट समूह को बाध्य किए बिना सार्वभौमिक रूप से इसके अनुप्रयोग से संबंधित हैं, सामान्य कानून हैं। ये कानून प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए नियंत्रित करते हैं और प्रकृति में सिविल हैं। ऐसे कानून या तो वैधानिक, प्रक्रियात्मक या मूल कानून हो सकते हैं।

स्वीय कानून
स्वीय कानूनों को उन कानूनों के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के विवाह, विरासत, तलाक, संरक्षकता, वसीयत आदि के मामलों को स्पष्ट करते हैं। ये कानून एक-दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये कानून विशेष रूप से व्यक्तियों के एक निश्चित समूह पर लागू होते हैं। स्वीय कानून अधिकतर प्रथागत कानून हैं, क्योंकि रीति रिवाज उनके प्राथमिक स्रोतों में से एक है। भारत में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936, और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 प्रचलित हैं और ये स्वीय कानून के कई उदाहरणों में से कुछ हैं।
हिंदू कानून की उत्पत्ति
हिंदू कानून इतिहास की किताबों में सबसे पुराने सभ्य कानूनों में से एक है। लगभग 2500 वर्षों की प्राथमिक उत्पत्ति से उपजे स्रोतों के साथ, हिंदू कानून को सबसे प्राचीन कानून माना जाता है। प्राथमिक स्रोत 500 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ थे, जिन्हें धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इन शास्त्रों को दैवीय रहस्योद्घाटन (रिवीलेशन) माना जाता था, जो वेदों का भी हिस्सा बन गए। वेद धार्मिक ग्रंथों का एक संकलित निकाय हैं जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं में प्रमुख हैं, जो प्रथागत कानूनों के रूप में मौलिक सिद्धांतों को स्थापित करते हैं।
वर्ष 1772 में अंग्रेजों ने आंग्ल-भारतीयों (एंग्लो-इंडियन) के लिए धर्मशास्त्रों को हिंदू कानून के दायरे में लागू करने का प्रयास किया। उनकी यह राय थी कि भारतीय लोगों पर अंग्रेजी कानून थोपने से वे ऐसे कानूनों का पालन करने से विमुख हो जायेंगे। इससे औपनिवेशिक (कोलोनियल) कानूनों के साथ-साथ न्यायिक उदाहरणों में हिंदू दर्शन को लागू किया गया। सर विलियम जोन्स, जिन्होंने 1783-1794 के आसपास बंगाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, हिंदू दर्शन से आकर्षित हुए और उन्होंने अपने निर्णयों में उन्हें लागू करने के लिए सार पुस्तिका (डाइजेस्ट) और टिप्पणियों से ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए संस्कृत सीखी। आंग्ल-भारतीयों कानून का निर्माण इस बात का एक और उदाहरण हो सकता है कि हिंदू दर्शन ने औपनिवेशिक शासकों को कैसे प्रभावित किया।
धीरे-धीरे, 1955-56 के आसपास, कानून निर्माताओं ने विवाह, उत्तराधिकार, अल्पवयस्कता (माइनॉरिटी) और संरक्षकता, और दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) और भरण पोषण के संबंध में कानून जैसे धार्मिक रूप से प्रेरित सिद्धांतों को शामिल करने का निर्णय लिया। ये अनेक विधायी अधिनियम दर्शाते हैं कि हिंदू कानून का क्षेत्र कितना विविध है। इस लेख में बाद में लेखक ने सबसे प्रचलित क़ानूनों पर विस्तार से चर्चा की है।
हिंदू कानून की उत्पत्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से दो विचार हैं, जो हैं; दैवीय उत्पत्ति, हिंदुओं द्वारा समर्थित और उनकी आस्था और; पश्चिमी न्यायविदों द्वारा माने जाने वाले प्रथागत कानून। इन विचारों का विस्तार निम्नलिखित है:
दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत
माना जाता है कि हिंदू कानून की उत्पत्ति से संबंधित यह वर्गीकरण दैवीय उत्पत्ति, यानी वेदों के पाठों से लिया गया है। ऐसे ग्रंथों को देवत्व का रहस्योद्घाटन माना जाता है और बाद में इसे लिखित शिल्प में बदल दिया गया, जिसने हिंदू कानून की शिक्षाओं को पीछे छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि दैवीय शिक्षाएँ अपौरुषेय हैं, जिसका तात्पर्य मानव उत्पत्ति से नहीं है। यह दृढ़ता से माना जाता है कि वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के रहस्योद्घाटन ने कुछ शिक्षाएं और दर्शन प्रदान किए हैं जिन्हें हिंदू कानून के दायरे में आत्मसात किया गया है।
वेदों और स्मृतियों के पवित्र ग्रंथों से प्राप्त शिक्षाओं में नैतिक और सामाजिक आचरण, कानूनी सिद्धांत और जीवन के दर्शन शामिल हैं। इन पाठों को हिंदू कानूनी न्यायशास्त्र में प्रदान किया गया माना जाता है, जिसे बाद में प्रख्यात विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा लिखी गई विभिन्न टिप्पणियों और सार पुस्तिका के माध्यम से प्रमाणित किया गया।
प्रथागत उत्पत्ति सिद्धांत
हिंदू कानून के स्रोतों का यह वर्गीकरण पश्चिमी न्यायविदों और हिंदू कानूनी दर्शन के अभ्यास में प्रथागत प्रथा को शामिल करने के संबंध में उनकी राय से उभरा है। पश्चिमी न्यायविद पवित्र ग्रंथों या दैवीय रहस्योद्घाटन में दृढ़ विश्वास नहीं रखते थे और प्रथा के अभ्यास और प्रचलित रीति-रिवाजों पर निर्भर थे। ऐसा माना जाता है कि भारत में आर्यों की स्थापना के समय, वे कुछ प्रथा को रीति-रिवाजों के रूप में स्वीकार करते थे और मानदंडों के रूप में उनका पालन करते थे, जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा और संशोधित किया गया था।
पश्चिमी संस्कृति के न्यायविदों की यह राय थी कि एक निश्चित समूह या समुदाय के बीच प्रचलित प्रथा हिंदू कानून के सिद्धांतों का मूल सिद्ध होती हैं। वे प्रथा को कानून मानते थे, क्योंकि प्रकृति प्रथागत थी जो हिंदू कानूनी न्यायशास्त्र के साथ समानता को दर्शाती थी।
हालाँकि, इस सिद्धांत की हेनरी मेन द्वारा अवहेलना की गई, जो मानते थे कि हिंदू कानून प्रथागत कानूनों की सबसे पुरानी वंशावली में से एक है, जो प्राचीन धर्मग्रंथों और पवित्र ग्रंथों के माध्यम से शासित होता है। उन्होंने आगे प्रदर्शित किया कि विवाह और तलाक, विरासत, अल्पवयस्कता और संरक्षकता, कुटुंब मामले, दत्तक ग्रहण आदि से संबंधित स्वीय कानून विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से अच्छी तरह से स्थापित हैं, जो दिव्य रहस्योद्घाटन के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
हिंदू कानून के संप्रदाय
हिंदू कानून के संप्रदायों के उद्भव का पता पवित्र धर्मग्रंथ की व्याख्या की आवश्यकता और किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय में प्रचलित विभिन्न रीति-रिवाजों और प्रथाओं को वर्गीकृत करने से लगाया जा सकता है। “संप्रदायों” का सिद्धांत मिताक्षरा और दयाभागा से विकसित हुआ, जिन्हें ब्रिटिश प्रशासन के एक घटक के रूप में माना जाता था, जो उसी को संहिताबद्ध (कोडिफाई) करने के लिए हिंदू कानूनी परंपरा को रेखांकित करने के प्रयास के परिणामस्वरूप हुआ था।
अंग्रेजों के शासन से पहले, संहिताबद्ध हिंदू कानूनों के एक समूह की आवश्यकता थी। हिंदू कानून पूरी तरह से प्रथागत कानूनों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था, जो शोधकर्ताओं द्वारा व्याख्या के अधीन था। ‘संप्रदाय’ शब्द को सबसे पहले एच.टी. कोलब्रुक, जो एक ब्रिटिश विद्वान और शोधकर्ता थे, द्वारा प्रयोग किया गया था। उन्होंने अपने शोध से पूरे देश में विभिन्न व्याख्याओं की खोज की, जिन्हें उन्होंने ‘संप्रदाय’ कहा।
मिताक्षरा
हिंदू कानून का मिताक्षरा संप्रदाय दो महत्वपूर्ण कानूनी परंपराओं में से एक है, जो मूल रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टिप्पणी के लिए जाना जाता है, जिसके लेखक विज्ञानेश्वर थे, जो 11वीं सदी के विद्वान थे। यह संप्रदाय पश्चिम बंगाल और असम राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में व्यापक रूप से लागू है। हालाँकि, इसके विभिन्न प्रथागत नियमों के कारण इसका अभ्यास क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न उप-संप्रदाय और न्यायिक विरोधाभास होते हैं।
मिताक्षरा संप्रदाय के संदर्भ में, संपत्ति सहदायिकों (कॉपर्सनर) यानी संयुक्त उत्तराधिकार के माध्यम से, के पास होती है और बेटे के अधिकार जन्म से विरासत में मिलते हैं। संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक का हिस्सा अन्य सहदायिकों के जन्म या मृत्यु के कारण घटता-बढ़ता रहता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कोई निश्चित या पूर्ण अधिकार नहीं है। मिताक्षरा प्रणाली वंश की चौदहवीं डिग्री तक समान उत्तराधिकार का समर्थन करती है। हिंदू कानून के मिताक्षरा संप्रदाय को पांच उप-संप्रदायों में विभाजित किया गया है, जिनकी संक्षेप में चर्चा इस प्रकार है:

बनारस कानून संप्रदाय
हिंदू कानून का बनारस संप्रदाय, जिसे वाराणसी या काशी संप्रदाय भी कहा जाता है, मिताक्षरा परंपरा द्वारा शासित महत्वपूर्ण उप-संप्रदायों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। यह उप-संप्रदाय विरमित्रोदय, विवाद और निर्णयसिंधु द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख टिप्पणियों से शिक्षाओं को एकीकृत करता है। बनारस संप्रदाय सहदायिक और संयुक्त परिवार की संपत्ति से संबंधित अवधारणाओं पर जोर देता है, जो जन्म से पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाले पुरुष वंशजों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर उप-संप्रदाय से तुलना की जाए तो बनारस संप्रदाय मिताक्षरा सिद्धांतों का बारीकी से पालन करता है, जिसमें पुरुष उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत पर जोर दिया जाता है।
मिथिला कानून संप्रदाय
मिथिला कानून संप्रदाय ज्यादातर तिरहुत और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में प्रचलित है। यह संप्रदाय विवादरत्नाकर, विवादचिंतामणि और स्मृतिसार की टिप्पणियों पर केंद्रित है। मध्यकाल में संतों और पुराने विद्वानों की शिक्षाओं और लेखों को औपचारिक रूप दिया गया। मिथिला संप्रदाय प्राचीन ग्रंथों और अनुष्ठानों के कड़े पालन के लिए प्रशंसित है, इसे कानूनी प्रथाओं में पारंपरिक समारोहों और रीति-रिवाजों पर महत्वपूर्ण जोर देने के लिए माना जाता है।
महाराष्ट्र या बॉम्बे कानून संप्रदाय
कानून का यह संप्रदाय गुजरात, कैराना और अन्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार क्षेत्र रखता है, खासकर जहां मराठी व्यापक रूप से बोली जाती है। व्यवहार मयूख और वीरमित्रोदय के ग्रंथ इसके प्रमुख प्रामाणिक ग्रंथों में से एक हैं। हिंदू कानून का यह संप्रदाय दूर के रिश्तेदारों (महिला बंधुओं) को वैध उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करता है। महिला बंधुओं या दूर के रिश्तेदारों के समूह में सगोत्र (एग्नेट) और सजातीय (कॉग्नेट) दोनों शामिल होते हैं, जो एक सामान्य पूर्वज से रिश्तेदारी के पांच डिग्री के भीतर के रिश्तेदारों तक विस्तारित होते हैं, इसमें वे व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो महिला वंश से जुड़े होते हैं।
मद्रास कानून संप्रदाय
मिताक्षरा संप्रदाय का यह वर्गीकरण भारत के पूरे दक्षिणी क्षेत्र को शामिल करता है और मिताक्षरा कानून संप्रदाय द्वारा प्रशंसित सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। यह स्मृति चंद्रिका, पराशर माधवीय और वीरमित्रोदय जैसे आधिकारिक ग्रंथों से काफी हद तक निकला है। मिताक्षरा इसका प्राथमिक स्रोत है, अन्य कार्य संप्रदाय के भीतर महत्व रखते हैं।
मद्रास संप्रदाय आम तौर पर महिलाओं को विरासत से बाहर रखने के वैदिक सिद्धांत का सख्ती से पालन करता था। इसने श्रुति के ग्रंथों की व्याख्या करते हुए सुझाव दिया कि बेटी, मां और महिलाओं के अलावा किसी भी महिला पूर्वजों को, जिन्हें स्पष्ट रूप से विरासत दी गई थी, संपत्ति प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं माना गया था। हालाँकि, समय के साथ, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त लोगों के अलावा अतिरिक्त महिला उत्तराधिकारियों को धीरे-धीरे विरासत के अधिकार दिए गए।
पंजाब कानून संप्रदाय
मिताक्षरा संप्रदाय का यह वर्गीकरण संप्रदाय की एक शाखा है, जिसका विकास मुख्यतः पूर्वी पंजाब में हुआ था। विराममित्रोदय इस संप्रदाय से जुड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक है। इसके अतिरिक्त, इस उप-संप्रदाय के निर्माण में क्षेत्र विशेष के स्थानीय रीति-रिवाजों का बहुत प्रभाव पड़ा।
मयूखा संप्रदाय
मयूखा संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार, उत्तराधिकार की प्रथा निकटता यानी रक्त संबंध के सिद्धांत पर आधारित है, जो दयाभाग संप्रदाय के सिद्धांतों के विपरीत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा कि मिताक्षरा संप्रदाय को उत्तराधिकारियों की श्रेणी में गर्भाशय बहन की स्थिति के बारे में समस्या का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, व्यवहार मयूखा स्पष्ट रूप से उत्तराधिकार के क्रम में बहन को दादी के ठीक बाद रखता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर मिताक्षरा संप्रदाय द्वारा किसी भी विनियमन की अनुपस्थिति की व्याख्या करते समय इस रुख को ध्यान में रखा।
दयाभाग
कानून का दयाभाग संप्रदाय मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में प्रचलित था और इसे हिंदू कानून के सबसे प्रमुख संप्रदायों में से एक माना जाता है। यह अपने सिद्धांतों को विभिन्न सार पुस्तिका और प्रमुख स्मृतियों से प्राप्त करता है, और अपना प्राथमिक ध्यान विरासत, विभाजन और संयुक्त परिवारों पर रखता है। पी.वी. केन, जो एक विद्वान, इतिहासकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य थे, ने स्थापित किया कि दयाभा संप्रदाय की उत्पत्ति 1090-1130 ईस्वी के बीच हुई थी। इस कानून की स्थापना पुरानी और कृत्रिम (आर्टिफिशियल) विरासत प्रथाओं को खत्म करने के लिए की गई थी।
इस संप्रदाय के मौलिक सिद्धांतों ने पहले के सिद्धांतों की अपर्याप्तताओं और प्रतिबंधों को संबोधित किया और सुधारा। संप्रदाय ने अंततः उत्तराधिकारियों की सूची का विस्तार करते हुए कई सजातीय लोगों को इसमें शामिल कर लिया, जिन्हें पहले हिंदू कानून के मिताक्षरा संप्रदाय के तहत बाहर रखा गया था। कानून का यह संप्रदाय कई प्रमुख टिप्पणियों से लिया गया था, जिसमें दयातत्य, दयाक्रम-संग्रह, विरमित्रोदय और दत्तक चंद्रिका शामिल हैं।
कानून का दयाभाग संप्रदाय स्वीय स्वामित्व की अवधारणा को मान्यता देता है, जहां एक संपत्ति विशेष रूप से किसी व्यक्ति के पास जीवन भर रहती है। दयाभाग प्रणाली के तहत, संपत्ति जन्म के बजाय मालिक की मृत्यु पर उत्तराधिकार द्वारा विरासत में मिलती है। यह घटना उत्तराधिकारियों को संपत्ति के निश्चित और विशिष्ट हिस्से प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। संपत्ति के मालिक की मृत्यु के बाद, एक स्वीय उत्तराधिकारी को हिंदू कानून की इस प्रणाली के तहत संपत्ति के विभाजन का अनुरोध करने का अधिकार है।
धर्म की अवधारणा
हिंदू न्यायशास्त्र के अनुसार, धर्म का अर्थ उन कर्तव्यों से है जिन्हें व्यक्ति को अपने जीवनकाल में निभाना होता है। संस्कृत शब्द ‘धर्म’ का शाब्दिक अर्थ ‘जीवन जीने का तरीका’ है। धर्म ‘पुरुषार्थ’ सिद्धांत के अंतर्गत चार अंतिम उद्देश्यों में से एक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘किसी व्यक्ति या आत्मा का अंतिम उद्देश्य’। अन्य तीन उद्देश्य हैं अर्थ (आर्थिक समृद्धि), काम (खुशी), और मोक्ष (आध्यात्मिक मुक्ति)। धर्म को इस ब्रह्मांड का संरक्षक, किसी के जीवन का अंतिम मार्ग और मनुष्य के चेतन और अवचेतन मन का नियंत्रक माना जाता है।
धर्म किसी विशेष धर्म से बंधा नहीं है बल्कि यह धार्मिक नियमों और कर्तव्यों का एक सार्वभौमिक समूह है। इसे किसी व्यक्ति के कानूनी कर्तव्यों का एक समूह कहा जाता है। विभिन्न धर्मों में धर्म का अलग-अलग अर्थ लगाया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार, धर्म ब्रह्मांडीय कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह, जैन धर्म में, धर्म तीर्थंकर की शिक्षाओं का प्रतीक है, जो व्यक्ति की शुद्धि को दर्शाता है।

जब हम कानून के संबंध में धर्म पर विचार करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि यह प्राकृतिक कानून की एक भारतीय शाखा है। न्यायशास्त्र के कानून के तहत प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को प्राचीन काल में हिंदू दर्शन में शामिल किया गया था, जिसका मैक्स मुलर जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने जोरदार समर्थन किया था।
धर्म की उत्पत्ति
कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, हिंदू धर्मग्रंथों और वेदों से हुई है। इसे अक्सर भगवद गीता की पवित्र पुस्तक में, दिव्यताओं द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शिक्षाओं में भी उद्धृत किया गया है। मेधातिथि की टिप्पणी के साथ मनुस्मृति के श्लोक 2.1 के अनुसार, धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “उस धर्म को सीखो, जिसका पालन, ज्ञानी और अच्छे लोगों के हृदय द्वारा किया गया है, जो प्रेम और घृणा से मुक्त हैं।” धर्मशास्त्रों के संदर्भ में, वशिष्ठ ने धर्म को इस प्रकार परिभाषित किया है, “धर्म वह है जो श्रुति और स्मृति में निहित है।”
ऐसी कई अन्य टिप्पणियाँ हैं जो श्रुति और स्मृति से उत्पन्न धर्म से संबंधित शिक्षाओं और ग्रंथों को चित्रित करती हैं। दोनों धार्मिक ग्रंथ हिंदू कानून के क्षेत्र में नैतिक और कानूनी व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं।
धर्म का स्वरूप
हिंदू न्यायशास्त्र के अंतर्गत अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। धर्म की प्रकृति विविध है और प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होती है: एक राजा को अपने राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, एक किसान का कर्तव्य फसल उगाना है, एक डॉक्टर को मनुष्यों को ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि एक वकील का कर्तव्य है अन्याय के खिलाफ लड़ना। प्रकृति में एक अत्यधिक धार्मिक अवधारणा होने के नाते, धर्म बहुआयामी है, जिसमें कानूनों और रीति-रिवाजों का एक व्यापक विस्तार शामिल है जो हिंदू कानून का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, मनुस्मृति में धर्म, प्रशासन, अर्थशास्त्र, सिविल और आपराधिक कानून, विवाह, उत्तराधिकार इत्यादि जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं, जो हमारे कानूनी ग्रंथों में शामिल मौलिक विषय हैं।
हिंदू कानून के स्रोत
हिंदू दर्शन प्राचीन काल के कई धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों से लिया गया है, और सदियों पुराने स्रोतों का पता लगाने के लिए, कई टिप्पणियां और सार पुस्तिका लिखे और अनुसरण किए गए हैं। हालाँकि, आधुनिक स्रोतों ने कानून, आधिकारिक मिसालों और समानता, न्याय और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति स्थापित की है। कानून का अस्तित्व सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और इसलिए, यह हमेशा इष्टतम है कि कानून को समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। कानून को समाज के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए।
हिंदू कानून के स्रोतों की खोज उन्नति के विभिन्न चरणों का अध्ययन है, जिसने इसे बढ़ाया और समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप इसमें रंग जोड़े। इसलिए, हिंदू कानून और उसके स्रोतों को काल के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित एक विस्तृत विश्लेषण है:
हिंदू कानून के प्राचीन स्रोत
वे स्रोत, जो रीति-रिवाजों, आध्यात्मिक या दैवीय ग्रंथों, पवित्र पुस्तकों के शिलालेखों (इनस्क्रिप्शन), सार पुस्तिका और प्राचीन ग्रंथों की टिप्पणियों के व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) हैं, हिंदू कानून के प्राचीन स्रोत हैं। उन्हें इस प्रकार संक्षिप्त किया जा सकता है:
श्रुति (वेद)
संस्कृत ‘श्रुति’ का शाब्दिक अर्थ है ‘जो सुना गया’। श्रुतियों को हिंदू कानून का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ऐसा कहा जाता था कि ऋषि मुनियों (ऋषियों) ने हिमालय पर्वत की चोटियों पर ध्यान किया और दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त किया, जिन्होंने आगे अपने शिष्यों को उन शिक्षाओं का उपदेश दिया। इस तरह के ज्ञान को फिर संकलित (कंपाइल्ड) और प्रलेखित (डोक्युमेंटेड) किया गया, जिसे बाद में वेदों के रूप में जाना गया। श्रुतियों को हिंदू कानून का प्राथमिक स्रोत माना जाता है।
वेद धार्मिक ग्रंथों का समूह हैं, जिन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: ऋग्वेद (अनुष्ठानों, बलिदानों और मंत्रों से संबंधित), यजुर्व वेद, सामवेद (जो धुनों और मंत्रों का संकलन है), और अथर्ववेद (जो वैदिक मंत्रों और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मंत्र, से संबंधित है)। ये वेद ज्ञान का भंडार हैं और इनमें से प्रत्येक में तीन भाग शामिल हैं: संहिता, जिसमें आध्यात्मिक भजन शामिल हैं; ब्राह्मणास, जिसमें कर्तव्यों और दायित्वों और उन्हें निष्पादित करने का उचित तरीका शामिल है; और उपनिषद, जो इन कर्तव्यों के सार को स्पष्ट करते हैं।
स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र
संस्कृत शब्द ‘स्मृति’ का शाब्दिक अर्थ ‘स्मृति’ या ‘जो याद किया जाता है’ है। स्मृति के ग्रंथ उन धारणाओं को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें ऋषियों ने अपनी स्मृतियों से दर्ज किया था। इन ग्रंथों को वेदों का खोया हुआ पाठ्य ग्रंथ माना जाता है, जो ऋषियों द्वारा प्राप्त दिव्य रहस्योद्घाटन से निकाले गए थे।
इस प्रकार स्मृतियों में कानून के निर्माण में मानवीय हस्तक्षेप शामिल है, जिसमें मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। कई प्रतिष्ठित संतों ने दिव्य रहस्योद्घाटन लिखे हैं; इनमें मनुस्मृति सबसे अधिक प्रचलित है। याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर और बृहस्पति जैसे कई अन्य प्रतिष्ठित संतों ने भी हिंदू कानूनी विचारों और नैतिकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए अपनी स्मृतियां अंकित की हैं। स्मृतियों को आगे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में वर्गीकृत किया गया है।
धर्मसूत्र ऐसे मैनुअल थे जो ऋषियों द्वारा अपने छात्रों को पढ़ाने के तरीकों का मार्गदर्शन करते थे। ये मुख्य रूप से 800 और 200 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए थे; शुरुआत में इसे गद्य (प्रोज) में तैयार किया गया था लेकिन बाद में इसमें छंद (वर्सेस) भी शामिल कर दिए गए। ये सूत्र स्थानीय रीति-रिवाजों और प्रथा के साथ वेदों का मिश्रण हैं और उन पर उनके लेखक का नाम अंकित है, ताकि यह पता चल सके कि वे किस शाखा से संबंधित हैं। धर्मसूत्र लिखने वाले कुछ प्रतिष्ठित ऋषि गौतम, बौधायन, आपस्तंब, हरिता, वशिष्ठ और विष्णु थे।
धर्मशास्त्र ऐसे ग्रंथ हैं जिनका पालन सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये ग्रंथ धर्मसूत्रों की तरह वेदों के बजाय पुराणों से लिए गए हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से छंदों में किया गया था, जो स्वयं धर्मसूत्रों से प्राप्त हुए थे। फिर भी, धर्मशास्त्र प्रकृति में अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित थे। इन ग्रंथों में आचार (धार्मिक आचरण), व्यवहार (सिविल कानून), और प्रायश्चित शामिल हैं।
मनुस्मृति
मनुस्मृति, जिसे वैकल्पिक रूप से ‘मनु के कानून’ कहा जाता है, हिंदू कानून के आयामों में सबसे विश्वसनीय ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह किसी व्यक्ति के सिविल आचरण संहिता और उनके द्वारा धर्म के संरक्षण को निर्धारित करता है। यह पाठ निर्धारित वर्गों या वर्णों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार संबंधी आचरण को भी रेखांकित करता है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। यह उन कानूनों की रूपरेखा भी बताता है जो नसिविल प्रकृति के हैं, जैसे अनुबंध और व्यवसाय।
मनुस्मृति पवित्र कानून के चार स्रोतों को मान्यता देती है। वे हैं- वेद, व्यक्तियों का सदाचार, पवित्र पुरुषों का आचरण और आत्म-प्राप्ति। ग्रंथों का दावा है कि इसके द्वारा निर्धारित सामाजिक कानून वेदों की शिक्षाओं के अनुरूप हैं। यह ‘राजधर्म’ की अवधारणा का भी प्रावधान करता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘शासन कला’। यह एक प्रांत पर शासन करने के तौर-तरीके और कौशल की पेशकश करता है।
मनुस्मृति के ग्रंथ जाति पदानुक्रम और महिलाओं के नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मनुस्मृति में अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध की रूपरेखा दी गई है और विवाह पर कानूनों के संबंध में कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मनुस्मृति के ग्रंथ अक्सर राजनीति, सामाजिक आचरण, धार्मिक रीति-रिवाजों और संबंधित नैतिकता, शासन कला और कई अन्य चीजों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
टिप्पणियाँ और सार पुस्तिका
टिप्पणियाँ और सार पुस्तिका प्रसिद्ध ऋषियों और मुनियों के दिव्य रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर लिखे और संकलित ग्रंथ हैं। किसी विशिष्ट स्मृति को विस्तृत करने के लिए किया गया कार्य भाष्य कहलाता है। इन टिप्पणियाँ का निर्माण 200 ईसा पूर्व के बाद हुआ था। सार पुस्तिका कानूनी लेखकों और विद्वानों द्वारा संक्षेप में श्रुति और स्मृति की विभिन्न लिखित सामग्रियों की एक रूपरेखा भी है।
ऐसे कई कार्य स्मृतियों में निहित विरोधाभासों से संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप कानून की एक उदार (लिबरल) व्याख्या हुई। मिताक्षरा और दयाभाग, हिंदू कानून के दो महत्वपूर्ण संप्रदाय, प्रख्यात विद्वानों की सार पुस्तिका और टिप्पणियों की शाखाओं से उभरे है।

रीति रिवाज
रीति-रिवाज को किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय तक अपनाई जाने वाली प्रथा या अभ्यास के रूप में माना जा सकता है। कई क्षेत्रों में रीति रिवाज का महत्व विधायी क़ानूनों से कहीं अधिक है। मूल रूप से, एक ऐसी प्रथा जो प्रकृति में प्राचीन है, नैतिक नीति और कानून के विपरीत नहीं है, उचित, निश्चित और स्पष्ट है, जो हमेशा से चलन में है, एक वैध रीति रिवाज है। रीति रिवाज शब्द को हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 की धारा 3 (a) के तहत परिभाषित किया गया है। हिंदू कानून के तहत कई सिद्धांत हैं जो रीति-रिवाजों से प्राप्त हुए हैं और अंततः कानून का रूप ले लिया है। स्मृतियों ने अपने ग्रंथों में रीति-रिवाजों के महत्व को भी रेखांकित किया है। स्मृतियों में वर्णित धर्मग्रंथ दर्शाते हैं कि रीति-रिवाज सर्वोपरि कानून हैं और ऐसी मान्यता पहले से ही मौजूद रही है।
एक वैध रीति रिवाज की अनिवार्यताएँ
- पुरातनता: किसी रीति रिवाज के वैध होने के लिए, उसका अनादि काल से होना और प्राचीन युग से संबंधित होना आवश्यक है। अनादि काल की धारणा इंग्लैंड के कानून से ली गई थी, जो कैनन कानून से प्रेरित थी। अनादि काल भी सिविल कानून का एक दृष्टिकोण है, जिसने इसकी व्याख्या इतनी दूर की अवधि के रूप में की कि किसी भी जीवित व्यक्ति को इसकी स्मृति नहीं होगी।
ठाकुर गोकलचंद बनाम परवीन कुमारी (1952) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘अनादि काल’ से अनुमानित अर्थ को स्पष्ट किया, और कहा कि “जनजाति के सदस्यों या परिवार” द्वारा इसके अस्तित्व के बारे में सामान्य साक्ष्य द्वारा एक रीति रिवाज को साबित किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि अंग्रेजी शासन को भारतीय कानूनी प्रणाली में लागू नहीं किया जा सकता है।
- तर्कसंगतता: एक वैध रीति रिवाज उचित होना चाहिए और नैतिक रूप से विरोधाभासी और अनुचित नहीं होना चाहिए। किसी रीति रिवाज की प्रकृति का पता उसके अस्तित्व और लोगों द्वारा उसकी स्वीकार्यता से लगाया जा सकता है। इसकी तर्कसंगतता की जांच करने के लिए, अदालत इसकी स्थापना पर वापस जा सकती है ताकि यह तय किया जा सके कि यह रीति रिवाज समाज या समुदाय के लिए फायदेमंद साबित हुई है या नहीं।
- निरंतरता: एक रीति रिवाज को वैध होने के लिए निरंतरता में होना चाहिए। एक वैध रीति रिवाज को समुदाय और ऐसे रीति रिवाज का पालन करने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इसकी स्थापना के समय से ही इस तरह के रीति रिवाज को बंद करने से इसकी वैधता ख़राब हो सकती है। मुहम्मद महमूद हुसैन फारूकी बनाम सैयद अब्दुल हक (1942) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक रीति रिवाज की निरंतरता पर जोर दिया और बताया कि यदि कोई रीति रिवाज लंबे समय से अस्तित्व में है और प्रचलित है तो एक सामान्य नियम को भी कैसे निरस्त किया जा सकता है। इस मामले में अदालत ने मामले की परिस्थितियों के आधार पर यह आवश्यक शर्त स्थापित की। इसने नेल्लोर की एक मस्जिद में खतीब के कार्यालय के क्रमिक मालिक की घोषणा करते हुए, परिवार के सदस्यों की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में हस्तक्षेप न करने पर प्रकाश डाला और इसे एक निर्बाध (अनइंटररेप्टेड) और वैध रीति रिवाज माना।
- निश्चितता: किसी रीति रिवाज के वैध होने के लिए उसे अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। निश्चित रूप से, इसका तात्पर्य यह है कि एक वैध रीति रिवाज सटीक, ठोस और स्पष्ट होने चाहिए। एक रीति रिवाज, यदि निश्चित नहीं है, तो उसकी प्रकृति और उद्देश्य से पता लगाया जा सकता है। रंगास्वामी गौंडन और अन्य बनाम अरुमुघा गौंडन (1936) के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि एक पेड़ की शाखाओं को पड़ोसी की भूमि पर लटकने की अनुमति देने वाले रीति रिवाज अस्पष्ट और अनिश्चित है। अदालत ने आगे कहा कि किसी पेड़ की शाखाओं को लटकाना एक उपद्रव (न्यूसेंस) होगा, जो कभी भी प्रथागत अधिकार नहीं बन सकता।
- वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप: यदि कोई रीति रिवाज किसी वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे मान्य नहीं किया जाता है। जहां प्रथागत कानून को कानून के स्रोतों के संबंध में कानून के बराबर माना जाता है, हालांकि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत इसे अप्रचलित घोषित किया जा सकता है।
कई देशों के विपरीत, भारत अपनी स्थिति पर कायम है कि कोई रीति रिवाज कभी भी क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। मोहम्मद बाकर और अन्य बनाम नईम-उन-निसा बीबी और अन्य (1955) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था। अदालत ने आगे कहा कि एक प्रथागत अधिकार किसी वैधानिक सिद्धांत को खत्म नहीं कर सकते जब तक कि ऐसा प्रथागत अधिकार पर्याप्त रूप से स्थापित न हो और लंबे समय से प्रचलन में हो।
- प्रकृति में अनिवार्य: एक समुदाय के लोगों द्वारा अपने अधिकारों के अभ्यास के रूप में एक रीति रिवाज को शामिल किया जाना चाहिए। इसे एक अधिकार के रूप में पहचाना जाना चाहिए, न कि जबरदस्ती की ताकत के रूप में। किसी रीति रिवाज को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए, इसे एक ऐसे दायित्व के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिसका स्वाभाविक रूप से पालन किया जाता है, न कि किसी बाहरी ताकत द्वारा मजबूर किया जाता है। हालाँकि, इस तरह का अनुपालन हमेशा गैर-जबरदस्ती प्रकृति का होना चाहिए।
- शांतिपूर्ण आनंद: किसी रीति रिवाज का शांतिपूर्ण और निर्बाध अभ्यास ऐसे रीति रिवाज को मान्य बनाता है। ऐसी धारणा है कि कोई भी रीति रिवाज ऐसी रीति रिवाज में भाग लेने वालों की सहमति से उत्पन्न होता है, और यदि इस रीति रिवाज को लंबे समय तक अदालत में चुनौती दी जाती है तो ऐसा सिद्धांत ख़राब हो जाएगा। इसलिए, एक रीति रिवाज को किसी भी प्रतिस्पर्धा से बाहर होना चाहिए और बिना किसी चुनौती के अपने अस्तित्व का आनंद लेना चाहिए
रीति रिवाज को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है
- स्थानीय रीति-रिवाज: जो रीति-रिवाज किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित हैं, उन्हें स्थानीय रीति-रिवाज के रूप में जाना जा सकता है। स्थानीय रीति-रिवाजों को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित लोगों के समूह द्वारा अपनाए जाने वाले नियमित संरचनात्मक पैटर्न के रूप में माना जा सकता है। प्रवास (माइग्रेशन) के मामले में स्थानीय रीति-रिवाज लोगों के साथ होते हैं। क्षेत्र में परिवर्तन से स्थानीय रीति-रिवाज की वैधता प्रभावित नहीं होगी। यह स्थानीय रीति-रिवाजों को भौगोलिक स्थानीय रीति-रिवाजों और स्वीय स्थानीय रीति-रिवाजों दोनों को शामिल करता है।
ये रीति-रिवाज तब तक वैध हैं जब तक वे सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जिनमें मुख्य रूप से प्राचीन होना भी शामिल है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुसम्मत सुभानी बनाम नवाब (1940) के मामले में फैसला सुनाया है कि एक रीति रिवाज लंबे समय तक प्रचलन में रहने से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, इसलिए उसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
- पारिवारिक रीति-रिवाज: जो रीति-रिवाज एक परिवार में लंबे समय से प्रचलित हैं, उन्हें पारिवारिक रीति-रिवाज के रूप में रखा जा सकता है। ऐसी पारिवारिक परंपराएँ, यदि किसी वैध रीति-रिवाज की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप साबित होती हैं, तो उन्हें हिंदू कानून के तहत कानून के रूप में मान्यता दी जा सकती है। बिकल चंद्र गोप और अन्य बनाम मंजुरा गोवालिन और अन्य (1972) के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि एक परिवार द्वारा लंबे अंतराल के लिए लागू किए गए रीति-रिवाजों को वैध स्वीय कानून माना जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय ने यह भी उद्धृत किया कि, “हिंदू कानून केवल एक स्थानीय कानून नहीं है बल्कि स्वीय कानून है और हर परिवार की स्थिति का हिस्सा है जो इसके द्वारा शासित होता है।”
- जाति और सामुदायिक रीति-रिवाज: ये रीति-रिवाज एक विशिष्ट जाति या समुदाय द्वारा प्रचलित हैं और ऐसे समुदाय या जाति के सदस्यों के लिए अनिवार्य हैं। हालाँकि, उन्हें वैध रीति रिवाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, दक्षिणी भारत में, अधिकांश तमिलनाडु में, कुछ समुदाय सजातीय विवाह का अभ्यास करते हैं; चाचा-भतीजी की शादी। इस अनुष्ठान को ‘मामन कल्याणम’ कहा जाता है, और यह परिवार में बेटी की वापसी के सिद्धांत पर आधारित है। हालाँकि, आज के युग में, कई सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के कारण, ऐसे रीति-रिवाजों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है।
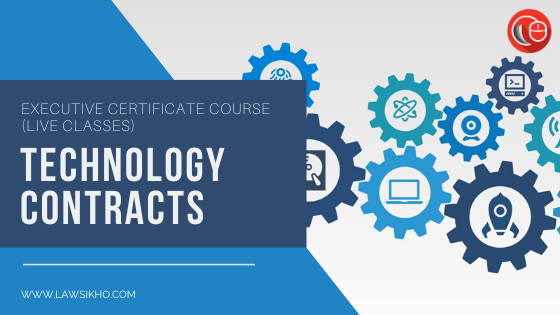
हिन्दू कानून के आधुनिक स्रोत
हिंदू कानून को प्रथागत और विधायी कानून का मिश्रण माना जाता है। यह दोनों प्रकार के कानूनों की एक शाखा है, जो एक निकाय में संरचित है। हिंदुओं के दायरे में लागू कानूनों के मुख्य आधुनिक स्रोत हैं; न्यायिक निर्णय, कानून, न्याय, समानता और अच्छा विवेक। ये तीन स्तंभ संहिताबद्ध कानूनों के साथ हिंदू कानूनी परिदृश्य को आकार देते हैं। इनमें 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 का हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और कई अन्य शामिल हैं। इसी तरह, न्यायिक मिसालें मौजूदा कानूनों की व्याख्या करने और नए बाध्यकारी कानूनों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी भी मौजूदा कानून के अभाव में, न्याय, समानता और अच्छा विवेक सामने आता है।
न्यायिक मिसालें
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को बाध्यकारी और देश का कानून मानने का आदेश देता है। तदनुसार, कई न्यायाधीश-निर्मित कानून व्यापक और अनिवार्य कानूनों में विकसित हो गए हैं। समय के साथ, मिसालों ने टिप्पणियों को खत्म कर दिया है, और उन्हें अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की शुरुआत से पहले, प्रिवी काउंसिल द्वारा कई पहलुओं को संशोधित किया गया था। इनमें दत्तक ग्रहण के कानून, हिस्से को अलग करने की सहदायिक की शक्तियां, महिलाओं के अधिकारों को बताना, स्त्रीधन और बहुत कुछ शामिल हैं।
न्यायिक मिसालों को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है
- मूल और घोषणात्मक: किसी फैसले या निर्णय को मूल मिसाल कहा जा सकता है जब ऐसे निर्णय का निर्णय का औचित्य हाल ही में सतह पर आया हो। मूल मिसालों को औपचारिक रूप से ‘न्यायाधीश-निर्मित कानून’ कहा जाता है जिन्हें बाद में संदर्भ के रूप में मामलों में अवधारणाबद्ध (कॉन्सेप्चुअलाइज़्ड) किया जाता है।
जबकि, घोषणात्मक मिसालें वे हैं जो मौजूदा और पहले से स्थापित कानूनी सिद्धांतों को लागू करती हैं। घोषणात्मक मिसालें कानून के स्रोत के रूप में गठित नहीं होती हैं, जबकि मूल मिसाल को मूल सिद्धांत कहा जाता है।
- आधिकारिक या प्रेरक (परस्यूएसिव): आधिकारिक मिसालें वे हैं जो आधिकारिक अदालतों द्वारा पारित की जाती हैं और जो निचली अदालतों पर बाध्यकारी होती हैं। इन मिसालों को बाध्यकारी कानून माना जाता है।
दूसरी ओर, प्रेरक मिसालें वे हैं जो प्रकृति में सम्मोहक हैं लेकिन अनिवार्य नहीं हैं। एक अदालत ऐसे मिसालों से प्रेरणा ले सकते है जो प्रकृति में प्रेरक हैं और महान उदाहरण स्थापित करते हैं, सिद्धांतों की स्थापना करते हैं।
विधान
अपनी संहिताबद्ध प्रकृति के कारण हिंदू कानून को सबसे विकसित और उन्नत स्वीय कानूनों में से एक कहा जाता है। समकालीन हिंदू कानून कई विधायी अधिनियमों और न्यायिक मिसालों का परिणाम है जिन्होंने इसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। कानून ने कुछ पारंपरिक पाठ्य कानूनों को सुधारने और यहां तक कि उन्हें बदलने में मदद की है। ब्रिटिश काल से पहले, हिंदू कानून अपनी विविध टिप्पणियों और सार पुस्तिका के कारण हिंदू के विभिन्न संप्रदायों में भिन्न था। वैधानिक अधिनियमों के प्रारंभ होने से कानूनों में एकरूपता के साथ-साथ उनकी अनुप्रयोगयता भी आती है। जातीय विकलांगता निवारण अधिनियम, 1850, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856, भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, संरक्षक और प्रतिपाल्य (वार्ड) अधिनियम, 1890, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929 (शारदा अधिनियम) जैसे अधिनियम हिंदू कानून के आधुनिकीकरण में परिवर्तनकारी उपकरण साबित हुए हैं।
ये अधिनियम उस कानून के उत्पाद हैं जो सिविल प्रकृति के मुद्दों के लिए प्रावधान और दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं। इस कानून ने भारतीय कानूनी प्रणाली को आकार देने में एक मार्ग प्रशस्त करने में मदद की है जिससे सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने में तेजी आई है।
जाति विकलांगता निवारण अधिनियम, 1850 कठोर जाति-आधारित अत्याचारों को खत्म करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम था। इस अधिनियम ने जाति और नस्ल के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव न करना सुनिश्चित किया। इसने जाति और नस्ल की परवाह किए बिना संपत्ति अर्जित करने और कानूनी उपायों तक पहुंच की अनुमति दी।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने पूरे भारत में महिलाओं की कानूनी और सामाजिक स्थिति सुनिश्चित की। इस अधिनियम ने महिलाओं की कानूनी स्थिति को तर्कसंगत बनाया, जो कि ज्यादातर समाज के पितृसत्तात्मकता में खो गई है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, विधवाओं को समाज में सामाजिक बहिष्कार और उपेक्षा का सामना करना पड़ता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, और समाज में बुनियादी सामाजिक स्थिति से परहेज किया जाता था।
वर्ष 1875 में स्थापित भारतीय वयस्कता अधिनियम, कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हुआ जिसने उम्र और वयस्कता के कानूनों से संबंधित एक संहिताबद्ध संरचना प्रदान की। यह क़ानून किसी प्राणी की वयस्कता की पहचान करने के लिए एक समान कानूनी मानकीकृत संहिता प्रदान करता है।
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ने संपत्ति से संबंधित कानूनों के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया है, जिसमें संपत्ति के पांच प्रकार के हस्तांतरण शामिल हैं, जो हैं; बिक्री, बंधक (मॉर्गेज), पट्टा (लीज), विनिमय (एक्सचेंज) और उपहार। इस कानून ने संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित मूल और प्रक्रियात्मक कानूनों का विस्तृत मसौदा तैयार करना सुनिश्चित किया।
संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, जो वर्ष 1890 में शुरू हुआ, बच्चों और उनके मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है। इसका संबंध उन बच्चों से है जो असुरक्षित और अलग-थलग हैं। संरक्षकों और प्रतिपाल्यों की नियुक्ति में संपत्ति की जांच के बाद अदालत की कार्यवाही शामिल होती है।
1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ने 14 वर्ष (लड़कियों के लिए) और 18 (लड़कों के लिए) से कम उम्र में विवाह पर रोक लगाकर बच्चों (लड़की और लड़के दोनों) की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार की। यह क़ानून समाज की एक सामाजिक बुराई, जो कि बाल विवाह है, को ख़त्म करने में अग्रणी साबित हुआ। इस अधिनियम में कहा गया है कि एक बच्चा इतना परिपक्व (मैच्योर) हो कि वह विवाह संस्था जैसी बड़ी ज़िम्मेदारी की प्रकृति और परिणामों को समझ सके।
न्याय, समानता और अच्छा विवेक
न्याय, समता और विवेक का प्रयोग कानून के अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। इसलिए, हिंदू कानूनों के निर्माण में इसकी उपस्थिति एक अपरिहार्य (इनएविटेबल) तत्व है। इन अवधारणाओं की शुरुआत का पता आधुनिक अंग्रेजी न्यायाधीशों के समय से लगाया जा सकता है, जब उन्हें न्याय और समानता के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई, विशेष रूप से किसी भी लागू कानून की अनुपस्थिति में या विरोधाभासी प्रावधानों के दौरान।
न्याय, समानता और अच्छे विवेक की अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में वर्ष 1606 में हुई, जब कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट की स्थापना की गई थी। अदालतों के आयुक्त ने न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों को लागू करते हुए मामलों के निपटान का आदेश दिया। हालाँकि, भारत में इस तरह के सिद्धांत का प्रयोग वर्ष 1780 में बंगाल की अध्यक्षता के दौरान शुरू किया गया था।
सर एलिजा इम्फ़े, जो कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के अग्रणी मुख्य न्यायाधीश थे, ने महत्वपूर्ण दिशानिर्देश लागू किए जो आज की तारीख में भी अपना स्थान पाते हैं। उन्होंने कहा कि, उन परिस्थितियों में जहां मामलों के संबंध में संहिताबद्ध या स्पष्ट प्रावधानों का अभाव है, मुफस्सिल और सदर अदालतों को न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों को लागू करते हुए संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया था।
इस तरह के कार्यान्वयन ने अदालतों को न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत के आधार पर, संबंधित प्रावधानों के अभाव में भी मुद्दों को संबोधित करने के लिए मजबूर किया। अदालतों ने यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया कि न्यायिक प्रणाली में कोई खामी न रह जाए और पर्याप्त कानून के अभाव के कारण किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो।
न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर ने एक बार एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि भारतीय कानूनी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों में न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच विचारधाराओं को अलग करने के लिए यह ज्ञान दिया।
न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत प्रकृति में आयामी और बहुआयामी हैं और अनंतिम कानूनों से परे अपने क्षेत्र को फैलाने की क्षमता रखते हैं। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का एक बड़ा दायरा प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय की कई व्याख्याओं ने क़ानून और संविधान की व्याख्या के दायरे को व्यापक बना दिया है।
एम. सिद्दीक एवं अन्य बनाम महंत सुरेश दास और अन्य के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की कि अनुच्छेद 142 न्याय, समानता और अच्छे विवेक की सीधी व्याख्या है। इसने आगे देखा कि, हालांकि सिद्धांत का कोई प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं है या अदालत को अपने सभी मामलों में प्रावधान लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, कई संवैधानिक प्रावधान इसे अपनी व्याख्या, दायरे या संदर्भ के माध्यम से आत्मसात करते हैं। अनुच्छेद 32, 136, और 226 न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावशाली तरीका पेश करते हुए न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांत को शामिल करते हैं।
हिंदू कौन हैं?
प्राचीन पुस्तकों में ‘हिन्दू’ की कोई सख्त परिभाषा नहीं दी गई है। हालाँकि, ‘हिंदू’ शब्द यूनानियों की शुरुआत से उभरा, जिन्होंने सिंधु घाटी के निवासियों को ‘इंडोई’ कहा और धीरे-धीरे प्रसिद्ध हो गया। हालाँकि, इसकी कोई सख्त परिभाषा नहीं है, लेकिन, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अधिनियमन के बाद, अधिनियमों के लागू होने की भावना है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 2(1)(a) और (b) के तहत एक अनंतिम परिभाषा निर्धारित करता है। धारा 2(1)(a) के अनुसार, उस व्यक्ति को धर्म से हिंदू कहा जाता है जो वीरशैव, लिंगायत का अनुयायी (फॉलोवर) है, या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज का अनुयायी है, जबकि धारा 2(1)(b) के तहत हिंदुओं के दायरे में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो धर्म से बौद्ध, सिख और जैन हैं। धारा आगे बताती है कि जो व्यक्ति मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है वह हिंदू है। हिंदू कौन है, इसके संबंध में समान रूप से संरचित परिभाषा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(1), हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 3, और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 2 के तहत भी प्रदान की गई है।

इसके अलावा, भारतीय संविधान ने हिंदू कौन है, इसके संबंध में एक कानूनी खंड प्रदान किया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25(2)(b) के स्पष्टीकरण II के तहत किया गया है। हिंदू कौन है की यह परिभाषा हिंदू कानून के विधायी क़ानूनों के तहत प्रदान की गई समान रूप से संरचित है।
कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में हिंदू धर्म का पालन करता है, चाहे अभ्यास करके या इसे स्वीकार करके, वह हिंदू है। हिन्दू धर्म बहुआयामी है इसलिए इसकी कड़ाई से व्याख्या करना एक असफल प्रयास है। हालाँकि, शास्त्री बनाम मुलदास भूरादास (1959) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ‘हिंदू’ को परिभाषित करने का निडर प्रयास किया और व्याख्या की कि हिंदू धर्म किसी एक दैवीय इकाई के इर्द-गिर्द नहीं घूमता है और किसी एक सिद्धांत का पालन नहीं करता है।
रूपांतरण द्वारा
पेरुमल बनाम पोन्नुस्वामी (1970), के मामले में हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य की एक व्याख्या निकाली गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया विवाह, जहां महिला पहले हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गई हो, वैध है। अदालत ने आगे कहा कि कोई व्यक्ति हिंदू बन सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से या अपने कार्यों से अपना इरादा व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में, रूपांतरण के इरादे को ध्यान में रखा जाना चाहिए और औपचारिक रूपांतरण या शुद्धिकरण की अनुपस्थिति रूपांतरण को ख़राब नहीं कर सकती है और उस व्यक्ति को हिंदू कहा जा सकता है। धर्म परिवर्तन के लिए व्यक्ति के पास नेक इरादा होना चाहिए और उसके पास धर्म परिवर्तन का कोई कारण भी नहीं होना चाहिए।
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2(1) का स्पष्टीकरण (c) यह प्रमाणित करती है कि “कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित या पुन: परिवर्तित होता है” वह हिंदू है। इस प्रकार, एक व्यक्ति जो हिंदू नहीं रह जाता है, वह हिंदू बन जाता है यदि वह हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख में से किसी एक में परिवर्तित हो जाता है। किसी अन्य धर्म से हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तन के कारण, कोई विशेष समारोह करना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि जिस जाति में रूपांतरण होता है, वह ऐसा करना अनिवार्य नहीं करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एस. अनबालागन बनाम बी देवराजन एवं अन्य (1983) मामले में माना था।
घोषणा द्वारा
टी. जी. मोहनदास बनाम कोचीन देवासम बोर्ड (1975) के मामले में केरल उच्च न्यायालय, पेरुमल मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित धारणाओं से एक कदम आगे निकल गया। केरल उच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी गलत इरादे या किसी अंतर्निहित मकसद के खुद को हिंदू घोषित करता है, तो उसे हिंदू कहा जाता है। गायक के जे येसुदास ने यह घोषणा करके कि वह हिंदू धर्म का पालन करते हैं, खुद को लैटिन कैथोलिक ईसाई से हिंदू में परिवर्तित कर लिया। रूपांतरण की ऐसी घोषणा एक वैध संबद्धता है।
जन्म द्वारा
आधुनिक हिंदू कानून के तहत, एक व्यक्ति दो शर्तों के तहत हिंदू होगा;
- यदि उसके माता-पिता दोनों हिंदू हैं
हिंदू माता-पिता दोनों से पैदा हुआ बच्चा हिंदू है। ऐसी स्थिति में जहां माता-पिता में से एक हिंदू है और दूसरा सिख या जैन या बौद्ध है, बच्चा हिंदू होगा। बच्चे के जन्म के समय माता-पिता की धार्मिक पहचान ही महत्वपूर्ण है। यदि माता-पिता में से कोई एक हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है, और बच्चे का पालन-पोषण उस धर्म के अनुसार किया जाता है, तो वह हिंदू नहीं रह सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2(1) के स्पष्टीकरण (a) में कहा गया है कि “कोई भी बच्चा, वैध या नाजायज, जिसके माता-पिता दोनों धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं;”
2. यदि उसके माता-पिता में से कोई एक हिंदू है और उसका पालन-पोषण हिंदू के रूप में हुआ है।
धारा 2 (1) के स्पष्टीकरण (b) प्रमाणित करता है कि कोई भी बच्चा, जो वैध या नाजायज हो सकता है, हिंदू कहा जा सकता है यदि उसके माता-पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है और ऐसे समुदाय या जनजाति के सदस्य के रूप में पाला गया है, जो इनमें से किसी एक धर्म की परंपराओं और संस्कृति का पालन करता है।
ऐसा अवश्य होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का पालन-पोषण ऐसे वातावरण में हुआ हो जहाँ ऐसे किसी भी धर्म की सांस्कृतिक नैतिकता और परंपराएँ प्रचलित और व्यवहार में थीं। हिंदू प्रथागत कानून का यह प्रावधान किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान निर्धारित करने में उसके पालन-पोषण और सामाजिक संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डालता है।
जन्म से हिंदू होने के नियम ऊपर बताए अनुसार ही रहेंगे; किसी व्यक्ति के जन्म के समय, उसके माता-पिता में से एक हिंदू था और उसका पालन-पोषण उस जनजाति के सदस्य के रूप में किया जाता है, जिससे उसके जन्म के समय हिंदू माता-पिता जुड़े हुए हैं। यह मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा मैना बोयी बनाम ऊटाराम (1861) के मामले में आयोजित किया गया था, जहां अदालत ने यह भी कहा था कि नाजायज बच्चों को हिंदू के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, और उनके अधिकारों को हिंदू कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए। यह मामला उन परिस्थितियों में हिंदू कानून की प्रकृति को दर्शाता है जहां बच्चे विवाह के बाहर भी पैदा होते हैं, यानी, हिंदू कानून हिंदू होने का दर्जा देता है यदि ऐसे व्यक्ति को ऐसे माहौल में लाया गया है जहां हिंदू रीति-रिवाज और परंपराएं प्रचलित हैं।
किन पर हिंदू कानून लागू नहीं होता
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(c) यह प्रमाणित करती है कि, कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र का निवासी है और मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का पालन नहीं करता है, वह हिंदू है। इसमें एक परंतुक (प्रोविजो) के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि, यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त चार धर्मों का पालन नहीं करता है, तो वे इस अधिनियम द्वारा शासित होंगे, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि इस अधिनियम के शुरू होने से पहले, वह व्यक्ति हिंदू कानून के अधीन नहीं रहा होगा।
अधिनियम की धारा 2(1) के स्पष्टीकरण (b) के अनुसार, हिंदू कानून उस बच्चे पर लागू नहीं होता, चाहे वह वैध हो या नाजायज, जिसके पिता हिंदू हैं और मां ईसाई है और बच्चा ईसाई समुदाय की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार पला-बढ़ा है। या फिर, एक हिंदू पिता और एक मुस्लिम मां की संतान, क्योंकि इस तरह के विवाह से उत्पन्न होने वाले बच्चे न तो जन्म से और न ही धर्म से हिंदू होते हैं। हिंदू कानून उन लोगों पर भी लागू नहीं होता है जो खुद को मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी में परिवर्तित कर लेते हैं, और उन हिंदुओं पर भी लागू नहीं होते हैं जो शास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं।

अधिनियम जिनके माध्यम से हिंदू कानून लागू होता है
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
विवाह, जिसे एक संस्कार इकाई माना जाता है, का तात्पर्य यह है कि यह पवित्र और अनुल्लंघनीय है। हिंदू धर्म के तहत, विवाह केवल औपचारिक अनुष्ठानों और रीति-रिवाजों के साथ ही पूरा होता है। मनु के अनुसार पति-पत्नी के बीच का बंधन अमर होता है और किसी की मृत्यु के बाद भी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। कई धार्मिक ग्रंथों और संहिताओं में पत्नी को पुरुष का आधा यानी अर्धांगिनी माना गया है। शतपथभ्रमण के अनुसार, “पत्नी पति का आधा भाग होती है।”
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 पत्नी और पति के विवाह के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लागू हुआ। यह अधिनियम विविध प्रकार के प्रावधान और अपवाद प्रदान करता है और इसमें विभिन्न समुदायों, परिवारों और लोगों के संप्रदायों को समायोजित करने की क्षमता है। अधिनियम का इरादा मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों को मजबूर करने के बजाय उनके हितों को संरक्षित करना और उनमें सामंजस्य स्थापित करना है। यहां तक कि यह शून्यकरणीय (वॉयडेबल) और शून्य विवाहों को भी समायोजित करता है, उनके लिए विशिष्ट प्रावधानों और अपवादों को निर्दिष्ट करता है। पहले, संसद का लक्ष्य हिंदू संहिता तैयार करना और चार क़ानूनों; हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956, और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 को संकलित करना था।
हिंदू विवाह अधिनियम के निर्माण को लेकर कानून निर्माताओं और हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायियों के बीच काफी विरोधाभासी राय देखी गई है। उन्हें डर था कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों को कानूनों में संहिताबद्ध करते समय पवित्रता से समझौता किया जा सकता है। संसद ने हिंदू संहिता में सभी महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करना सुनिश्चित किया, जिसमें रीति-रिवाजों, स्मृतियों और श्रुतियों के ग्रंथों और टिप्पणियों के एकीकरण पर जोर दिया गया। संसद ने कानूनों को शामिल करते हुए यह भी कहा कि हिंदू कानून बहुआयामी है और बदलते समय के साथ इसे विकसित करने की जरूरत है।
प्रख्यात टिप्पणीकारों द्वारा निभाई गई उल्लेखनीय भूमिका के साथ, विज्नेश्वर प्रमुखता से सामने आते हैं। प्रमुख परिवर्तनों में से एक हिंदू कानून के तहत दो संप्रदायों की शुरूआत द्वारा लाया गया था, जो हैं, मिताक्षरा और दयाभाग। दोनों सम्प्रदाय स्मृतियों और श्रुतियों की एक शाखा थे, तथापि, व्याख्याएँ भिन्न-भिन्न थीं। मिताक्षरा को आगे चार उप-संप्रदायों में विभाजित किया गया, जो हैं, बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्रविड़। हिंदू कानून का यह संप्रदाय जन्मस्वत्व (पैतृक स्वामित्व या जन्म से स्वामित्व) के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी ओर, दयाभाग बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी प्रचलित है। यह विचारधारा उपरामस्वत्वदा (मृत्यु के बाद उत्पन्न होने वाले वंशानुगत अधिकार या स्वामित्व) के सिद्धांत पर आधारित है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के महत्वपूर्ण घटक
व्याख्या खण्ड
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 हिंदू कानून में प्रचलित शब्दों की परिभाषाओं और व्याख्याओं से संबंधित है। यह प्रावधान ‘रीति-रिवाजों’ और ‘प्रथाओं’ को परिभाषित करता है, जो स्रोतों में से एक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रावधान उन खंडों को समायोजित करने का प्रयास करता है जो हिंदू कानून के क्षेत्र में अपरिहार्य हैं। धारा 3(c) ‘आधा-रक्त’ और ‘पूर्ण-रक्त’ को परिभाषित करती है। दो व्यक्तियों को आधा-रक्त संबंधी तब कहा जाता है जब उनके पूर्वज एक ही हों लेकिन उनके माता-पिता (माताएं) अलग-अलग हों। जबकि, ‘पूर्ण-रक्त’ एक सामान्य पूर्वज और एक ही माता-पिता (मां) के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाता है। इसी प्रकार, धारा 3(d) ‘गर्भाशय-रक्त’ को परिभाषित करती है, जो सामान्य पूर्वज और विभिन्न माता-पिता (पिता) के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संबंध को दर्शाता है।
इस खंड के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं में ‘सपिंडा संबंध’ शामिल है। यह उस रिश्तेदारी को संदर्भित करता है जो मातृ वंश की ओर तीन पीढ़ियों तक और पैतृक वंश की ओर पांच पीढ़ियों तक फैली हुई है। इसलिए, यदि इन मापदंडों के भीतर एक दूसरे का वंशज है, तो उसे दूसरे का सपिंड कहा जाता है। यह इस अधिनियम की धारा 3(f) के तहत प्रदान किया गया है।
वैध हिंदू विवाह के लिए शर्तें
हिंदू विवाह की वैधता इस अधिनियम की धारा 5 के तहत उल्लिखित कुछ मापदंडों पर विचार करके संपन्न की जाती है। इस अधिनियम के तहत छह प्रावधान हैं जो उचित हिंदू विवाह के गठन की शर्तों को काफी हद तक रेखांकित करते हैं।
- हिंदू विवाह के वैध होने के लिए, विवाह के दोनों पक्षों में से किसी का भी पहले से मौजूद जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। यह अधिनियम की धारा 5(i) के तहत प्रदान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है, तो दूसरी शादी अमान्य मानी जाएगी। यहां तक कि पहली पत्नी की सहमति भी उसके पति द्वारा की गई दूसरी शादी को मान्य नहीं करेगी। रतन चंद बनाम शांति देवी और अन्य (1998) के मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी यही व्यवस्था दी थी।
- इस अधिनियम की धारा 5(ii) किसी व्यक्ति को वैध हिंदू विवाह में पक्ष बनने की योग्यता प्रदान करती है। धारा 5(ii)(a) के तहत यह प्रावधान है कि हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए, विवाह में कोई भी पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण विवाह के लिए सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति शादी करने में सक्षम नहीं है, भले ही ऐसा व्यक्ति वैध सहमति देने में सक्षम हो, लेकिन वह इस हद तक मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित है कि वह बच्चों के प्रजनन के लिए अयोग्य प्रतीत होता है, जैसा कि धारा 5(ii)(b) के तहत प्रदान किया गया है। धारा 5(ii)(c) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो बार-बार पागलपन के हमलों से पीड़ित है, वह वैध विवाह के लिए सक्षम नहीं होगा।
- विवाह के दोनों पक्षों को वयस्कता की आयु प्राप्त करनी होगी। हालाँकि, दूल्हे के मामले में, न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष है। यह अधिनियम की धारा 5(iii) के तहत प्रदान किया गया है।
- अधिनियम की धारा 5(iv) के अनुसार, विवाह के पक्षों को निषिद्ध संबंधों के दायरे में नहीं आना चाहिए, जब तक कि पक्ष किसी विशेष समुदाय या जाति से न हों जहां ऐसी प्रथाओं को रीति-रिवाज के रूप में मान्यता दी जाती है।
धारा 3(g) उन रिश्तों को निर्दिष्ट करती है जो सपिंड हैं और निषिद्ध रिश्तों के अंतर्गत आते हैं। निषिद्ध संबंध के अंतर्गत व्यक्ति इस प्रकार हैं-
- यदि एक व्यक्ति दूसरे का वंशज है,
- यदि एक व्यक्ति दूसरे के वंशज या लग्न का पति या पत्नी है।
- यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाई, पिता या माता के भाई या दादा या दादी के भाई की पत्नी है।
- यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई या बहन, चाचा या भतीजी, चाची या भतीजा है। इसमें आगे कहा गया है कि यदि दो व्यक्ति एक भाई और बहन, या दो भाइयों या दो बहनों की संतान हैं तो एक व्यक्ति दूसरे का सपिंड है।
- अधिनियम की धारा 5(v) में कहा गया है कि दो व्यक्ति जो एक दूसरे के सपिण्ड हैं, विवाह में प्रवेश नहीं कर सकते। हालाँकि, ऐसा विवाह वैध है यदि इसकी अनुमति है और इसे एक रीति रिवाज के रूप में प्रचलित किया जाता है जो उन्हें नियंत्रित करती है।
लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में विवाह की वैधता अब न्यायिक रूप से प्रमाणित हो गई है। हालाँकि, एक जोड़े के रूप में निरंतर सहवास और प्रतिष्ठा स्थापित करने की आवश्यकता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने माणिक्यम बनाम अचम्मा (1953) 1 मैड एलजे 34 के मामले में भी यही व्यवस्था दी थी। कंचन मल्होत्रा बनाम यशवीर सिंह (1986), के एक अन्य मामले में भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि वैध हिंदू विवाह की धारणा पूरी तरह से सहवास पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें ‘आदत’ और ‘प्रतिष्ठा’ भी शामिल होनी चाहिए, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 50 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 44 के तहत प्रदान किया गया है। ऐसा विवाह उन व्यक्तियों के आचरण से साबित हो सकता है, जिन्हें परिवार के सदस्यों, दोस्तों या रिश्तेदारों के रूप में रिश्ते के बारे में विशिष्ट ज्ञान है।
शून्य एवं शून्यकरणीय विवाह
एक शून्य विवाह ऐसा है, जिसे पहले स्थान पर कभी भी वैध विवाह के रूप में संपन्न नहीं किया गया था, अर्थात, आरंभ से ही शून्य। इस अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाह के लिए प्रावधान करती है। यह धारा भावी (प्रॉस्पेक्टिव) प्रकृति की है और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद ही लागू होती है। यदि विवाह के दोनों पक्षों में से कोई भी धारा 5 (i), (iv), (v) का उल्लंघन करता है तो विवाह शून्य हो सकता है।
इसलिए, एक विवाह स्वतः ही शून्य हो जाता है यदि यह विवाह किसी पूर्व पति या पत्नी के अस्तित्व पर संपन्न हुआ हो और विवाह के पक्ष निषिद्ध संबंध की डिग्री के अंतर्गत आते हों या एक-दूसरे के सपिंड हों।
एक विवाह जिसे अदालत की डिक्री द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है, यदि विवाह का कोई भी पक्ष ऐसी डिक्री की मांग करता है, तो उसे शून्यकरणीय विवाह माना जाता है। अधिनियम की धारा 12 इस पहलू पर आधार, अपवाद और प्रावधान प्रदान करती है। यह प्रावधान प्रकृति में पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) है और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले विवाह में लागू होता है। शून्यकरणीय विवाहों के संबंध में दिए गए आधार इस प्रकार हैं।-
- यदि दूसरे पक्ष की नपुंसकता के कारण विवाह संपन्न नहीं होता है तो विवाह के दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा विवाह रद्द किया जा सकता है। इसका उल्लेख धारा 12(1)(a) के तहत किया गया है।
- यदि दूसरे पक्ष द्वारा धारा 5(ii) का उल्लंघन किया गया है, तो विवाह का कोई भी पक्ष अपनी शादी को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसमें कहा गया है कि यदि विवाह का कोई पक्ष मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण है और वैध सहमति देने में असमर्थ है, तो उसके पति या पत्नी के पास विवाह को रद्द करने का विकल्प होता है। यह धारा 12(1)(b) के तहत प्रदान किया गया है।
- जहां याचिकाकर्ता या उसके संरक्षक की सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की जाती है, विवाह शून्यकरणीय है और याचिकाकर्ता के विकल्प पर इसे रद्द किया जा सकता है, जैसा कि धारा 12(1)(c) के तहत उल्लिखित है।
- किसी विवाह में, यदि पत्नी पहले से ही अपने पति के अलावा किसी और से गर्भवती हो चुकी है, तो ऐसा विवाह पति के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है। यह धारा 12(1)(d) के तहत प्रदान किया गया है। हालाँकि, इसके संबंध में धारा 12(2)(b) के तहत उल्लिखित परंतुक है कि पति को अपनी पत्नी की गर्भावस्था के बारे में पता नहीं होना चाहिए, इस संदर्भ के आलोक में कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर शुरू होनी चाहिए (यदि ऐसा विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले हुआ हो) या विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर (यदि ऐसा विवाह अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद हुआ हो) और, वैवाहिक संभोग पति द्वारा गर्भावस्था के बारे में पता होने के बाद हुआ हो।
विवाह का पंजीकरण
इस अधिनियम की धारा 8 के माध्यम से विवाहों का पंजीकरण किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो हिंदू विवाह रजिस्टर में विवाहों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसा रजिस्टर इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए होगा और रिकॉर्डिंग नियमों और शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए। इसके अलावा, यदि राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए आवश्यक और लाभदायक समझी जाती है, तो विशिष्ट भागों में विवाहों की रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर सकती है। हालाँकि, सामान्य तौर पर, ऐसे विवाह की प्रविष्टि करने में चूक से विवाह कभी भी मान्य नहीं होगा।
तलाक
‘तलाक’ को अंग्रेजी में डायवोर्स कहते है यह शब्द लैटिन शब्द ‘डिवोर्टियम’ से निकला है, जिसका अर्थ है ‘अलग-अलग रास्ते’। यह एक पवित्र रिश्ते में दो पति-पत्नी के अलग होने को दर्शाता है। 1955 अधिनियम की शुरुआत के बाद से, इसमें दो संशोधन हुए हैं; हिंदू विवाह (संशोधन) अधिनियम, 1964, और विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976। हालिया संशोधन अधिनियम ने आपसी सहमति से तलाक के लिए एक नया आधार जोड़कर तलाक कानूनों के दायरे को उदार बना दिया है। अधिनियम की धारा 13 तलाक के लिए नौ आधार प्रदान करती है। विवाह का कोई भी पक्ष इस धारा में दिए गए आधारों के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए अदालत से मांग कर सकता है। आधारों को प्रमुख रूप से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है- दोष-सिद्धांत, विखंडन सिद्धांत, और पत्नी के लिए प्रदान किए गए आधार।

विवाह के बाहर यौन संबंध
इस आधार का उल्लेख धारा 13(1)(i) के तहत किया गया है, जो ‘व्यभिचार’ (एडल्टरी) का प्रावधान करता है। क़ानून में ‘व्यभिचार’ शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार, इसे ‘अपने जीवनसाथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध’ के रूप में दर्शाया जा सकता है। गीताबाई बनाम फट्टू और अन्य (1966) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ‘व्यभिचार’ की व्याख्या “एक विवाहित व्यक्ति और विपरीत लिंग के किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहमति से संभोग का एक कार्य है, जो पूर्व विवाह के अस्तित्व के दौरान उसका जीवनसाथी नहीं है।”
जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) के एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार के कार्य को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और आदेश दिया कि हालांकि व्यभिचार का आपराधिक आधार समाप्त कर दिया गया है, लेकिन सिविल प्रकृति के परिणाम अभी भी इससे संबंधित हैं। एक पत्नी अपने पति द्वारा किसी अन्य महिला, जो अविवाहित है, के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने के आधार पर अदालत से तलाक की डिक्री मांग सकती है।
क्रूरता
विवाह का कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा उस पर क्रूरता के आधार पर अदालत से तलाक की डिक्री की मांग कर सकता है, जिसका उल्लेख अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत किया गया है। क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। हालाँकि, मानसिक क्रूरता के मामले में, लंबी परिस्थितियों और घटनाओं के पर्याप्त सबूत होने चाहिए। क्रूरता को किसी के जीवन की सामान्य झगड़े से अलग करना होगा। इस आधार में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, नुकसान पहुंचाने की आशंका, हत्या की आशंका, शारीरिक शोषण, शारीरिक या मानसिक यातना, वश में करके यातना देना और बहुत कुछ शामिल हो सकता है।
वी. भगत बनाम डी. भगत (1994) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक क्रूरता के पहलू पर जोर दिया और माना कि मानसिक क्रूरता इतनी गंभीरता की होनी चाहिए कि यह पक्षों को एक-दूसरे और साथ रहने के लिए असहनीय बना दे। उन्होंने यह भी कहा कि जो बात एक मामले में क्रूरता हो सकती है, वह दूसरे में नहीं भी हो सकती है।
जीवनसाथी द्वारा परित्याग (डिजर्शन)
विवाह का कोई भी पक्ष, यदि उसके पति या पत्नी ने दो साल या उससे अधिक की लंबी अवधि के लिए उसे छोड़ दिया है, तो वह इस आधार पर उसे तलाक देने के लिए अदालत से अपील कर सकता है। यह आधार धारा 13(1)(ib) के तहत प्रदान किया गया है।
धर्म परिवर्तन
विवाह में एक पक्ष द्वारा धर्म परिवर्तन करने से विवाह स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाता है, दूसरे पक्ष को इस आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करनी होती है। हालाँकि, यदि कोई हिंदू रहता है तो विवाह को समाप्त करना पक्ष के विकल्प पर है। यह धारा 13(1)(ii) के तहत प्रदान किया गया है।
मन की अस्वस्थता
एक पक्ष अदालत से तलाक की डिक्री की मांग कर सकता है यदि उसका जीवनसाथी लाइलाज मानसिक बीमारी या मानसिक विकार से पीड़ित है जो सहवास को असंभव बनाता है। ऐसे मानसिक विकारों में सिज़ोफ्रेनिया भी शामिल है। इस प्रावधान में यह भी कहा गया है कि एक पक्ष के मनोरोगी विकार के मामले में, दूसरा पक्ष तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। मनोरोगी विकार असामान्य और अत्यधिक आक्रामकता को संदर्भित करेगा। इसका उल्लेख इस अधिनियम की धारा 13(1)(iii) के तहत किया गया है।
यौन रोग
विवाह का कोई भी पक्ष अपने पति या पत्नी के यौन रोग से पीड़ित होने के आधार पर तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए अदालत में अपील कर सकता है। ऐसा यौन रोग सामुदायिक और लाइलाज होना चाहिए। एसटीडी और एड्स जैसी यौन रोग जीवन के लिए खतरा हैं। इसलिए, दूसरा पक्ष स्वयं को विवाह से अलग करने का विकल्प चुन सकता है और उसे स्वस्थ और बीमारी से मुक्त रहने की स्वतंत्रता है। इसका उल्लेख धारा 13(1)(v) के अंतर्गत किया गया है।
संसार का त्याग
यदि उनके साथी ने धार्मिक क्षेत्र में शामिल होने के लिए दुनिया को त्याग दिया है तो पति या पत्नी अदालत से तलाक की मांग कर सकते हैं। यह आधार अधिनियम की धारा 13(i)(vi) के तहत उल्लिखित है।
मृत्यु का अनुमान
यदि कोई व्यक्ति कम से कम सात वर्षों तक नहीं मिला हो तो उसे मृत मान लिया जाता है। उसे तब मृत मान लिया जाएगा जब आसपास के लोगों जो स्वाभाविक रूप से उसे देखेंगे ने उसके बारे में नहीं सुना होगा या देखा नहीं होगा। पति-पत्नी मृत्यु की धारणा के आधार पर पुनर्विवाह कर सकते हैं और अदालत से तलाक मांग सकते हैं। इस आधार का उल्लेख इस अधिनियम की धारा 13(1)(vii) के तहत किया गया है।
पत्नी के लिए तलाक के आधार
द्विविवाह
एक पत्नी अपने पति जिसने द्विविवाह किया है, से तलाक लेने की हकदार है जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2)(i) में बताया गया है। हालाँकि, प्रावधान कुछ शर्तों को निर्धारित करता है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है, वे निम्नलिखित हैं-
- प्रश्न में विवाह, अधिनियम लागू होने के बाद होना चाहिए, और
- इसमें शामिल पति के पास दूसरी शादी करते समय पहले से ही एक जीवित जीवनसाथी होना चाहिए।
अधिनियम में एक दंड धारा का भी प्रावधान है, जिसका उल्लेख इस अधिनियम की धारा 17 के तहत किया गया है।
पति द्वारा बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार (सोडोमी) और पाशविकता (बेस्टीलिटी) का अपराध
यदि पति को बलात्कार, अप्राकृतिक यौनाचार या पाशविकता के अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो पत्नी को अधिनियम की धारा 13(2)(ii) के तहत तलाक लेने का अधिकार है। बलात्कार के अपराध को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 375 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 के तहत परिभाषित किया गया है। जबकि, अप्राकृतिक यौनाचार और पाशविकता के अपराध का उल्लेख भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 के तहत किया गया है।
भरण-पोषण की डिक्री जारी होने के बाद सहवास फिर से शुरू करने में विफलता
1976 के संशोधन अधिनियम ने महिलाओं के लिए तलाक मांगने के लिए एक और महत्वपूर्ण आधार शामिल किया। अधिनियम की धारा 13(2)(iii) में प्रावधान है कि, यदि पति के खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18, या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 144) के तहत भरण-पोषण की डिक्री या आदेश जारी किया गया था कि उसे पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करना होगा, और इस बीच, जोड़े ने डिक्री या आदेश के बाद एक वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास फिर से शुरू नहीं किया है, तो पत्नी तलाक के लिए दायर करने की हकदार है।
विवाह का खंडन
एक पत्नी को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर विवाह से इनकार करने के अधिकार के तहत तलाक की डिक्री के लिए अदालत से गुहार लगाने का अधिकार है। हालाँकि, उसे वयस्क होने से पहले इस अधिकार का पालन करना होगा।
आपसी सहमति से तलाक
विवाह के पक्ष आपसी सहमति से तलाक की डिक्री प्राप्त करने के लिए अदालत के समक्ष एक साथ याचिका दायर कर सकते हैं। हालाँकि, दोनों पक्ष एक वर्ष से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे होंगे और अपनी शादी को खत्म करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हुए होंगे।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
परिचय
भारत में संपत्ति का उत्तराधिकार और विरासत 1956 के अधिनियम द्वारा शासित होता हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संपत्तियों का वसीयतनामा उत्तराधिकार शामिल है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में, हिंदू महिलाओं के संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। इस विकास ने हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के भीतर महिला संपत्ति अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया। संशोधित 1956 अधिनियम में विधवा, माँ और बेटी को वर्ग 1 के उत्तराधिकारियों में शामिल किया गया। परिणामस्वरूप, एचयूएफ के भीतर विभाजन की स्थिति में, विधवा, बेटी और मां संपत्ति पाने की कतार में सबसे पहले होंगी।
अधिनियम के अनुप्रयोग
अधिनियम की धारा 2 इस क़ानून के अनुप्रयोग की गणना करती है। यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से हिंदू हैं और वीरशैव, लिंगायत, या ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज में विश्वास रखते हैं। यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो सिख, जैन और बौद्ध हैं। अधिनियम आगे दावा करता है कि इस क़ानून के तहत प्रावधान उन लोगों पर लागू हो सकते हैं जो ईसाई, मुस्लिम, यहूदी और पारसी नहीं हैं। हालाँकि, यह साबित होना चाहिए कि इस अधिनियम के अभाव में ऐसे लोग हिंदू कानून और रीति-रिवाजों द्वारा शासित होंगे।

इस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति की व्याख्या अधिनियम की धारा 2(1) के स्पष्टीकरण भाग के तहत प्रदान की गई है, जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रदान की गई व्याख्या के समान है।
यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अर्थ के भीतर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अपवाद निर्धारित करता है, जिसमें कहा गया है कि यह क़ानून जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का महत्वपूर्ण घटक
पुरुष निर्वसीयत उत्तराधिकार
मुख्य रूप से हिंदू पुरुषों के निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले नियम का उल्लेख हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 से धारा 13 में किया गया है। प्रावधानों का यह सेट उन मामलों में संपत्ति के हस्तांतरण को निर्धारित करता है जहां एक हिंदू पुरुष बिना वसीयत किए मर जाता है।
अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, एक हिंदू पुरुष की संपत्ति उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी, और इसकी अनुपस्थिति में श्रेणी ll के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जाएगी। श्रेणी II के उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति के अलावा, संपत्ति मृतक के रिश्तेदारों को हस्तांतरित की जाएगी, और रिश्तेदारों की अनुपस्थिति में, यह अंततः मृतक के रिश्तेदारों को हस्तांतरित की जाएगी।
अधिनियम की धारा 10 श्रेणी I के उत्तराधिकारियों के बीच पुरुष की संपत्ति के वितरण को विस्तृत करती है, जिसके अनुसार निर्वसीयत संपत्ति मृतक की विधवा को और फिर जीवित बेटे, बेटी और मृतक की मां को दी जाएगी। यह प्रावधान पूर्व-मृत पुत्रों और पूर्व-मृत पुत्रियों के मामलों और उनके उत्तराधिकारियों को संपत्ति के हस्तांतरण को और स्पष्ट करता है। जबकि, अधिनियम की धारा 11 श्रेणी II के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्तियों के बंटवारे का प्रावधान करती है।
अधिनियम की धारा 12 सगोत्र और सजातीयों के बीच उत्तराधिकार के क्रम पर जोर देती है, जो वरीयता के एक विशिष्ट नियम द्वारा निर्धारित होता है। कम उन्नति डिग्री वाले उत्तराधिकारी को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दो या दो से अधिक उत्तराधिकारियों के लिए उत्थान की डिग्री की संख्या समान है, तो कम वंश की डिग्री वाले उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि, उत्तराधिकारियों की डिग्रियों की गणना अधिनियम की धारा 13 के तहत निर्धारित की जाती है, जहां ऐसी डिग्रियों की गणना निर्वसीयत सहित की जाती है।
हिंदू महिला की संपत्ति
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है कि चल और अचल संपत्ति सहित सभी संपत्तियां जो एक हिंदू की हैं, जो महिला है, उसे केवल संपत्तियों के मालिक के रूप में रखा जाता है, न कि संपत्तियों के सीमित मालिक के रूप में। इन संपत्तियों में किसी के द्वारा उपहार में दिया जाना, खरीदा जाना, या शादी करते समय शामिल होना शामिल है। इस प्रकार, एक हिंदू महिला के पास अपनी संपत्तियों से निपटने की सर्वोच्च शक्ति है और वह अपनी संपत्तियों का निपटान अपनी इच्छा से कर सकती है, किसी को उपहार में दे सकती है, किसी को बेच सकती है और हस्तांतरण के अन्य तरीकों से कर सकती है।
हालाँकि, धारा 14(2) के अनुसार, महिला की संपत्ति पर कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। यदि किसी महिला के स्वामित्व वाली संपत्ति उपहार, वसीयत, किसी अन्य कानूनी दस्तावेज, अदालत की डिक्री या किसी पंचाट (अवॉर्ड) के माध्यम से अर्जित की जाती है, जिसमें अलगाव के लिए पुनः प्रशिक्षण की शर्तें शामिल हैं, तो ऐसी शर्तें मान्य होंगी।
महिला निर्वसीयत उत्तराधिकार
हिंदू महिलाओं के निर्वसीयत उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों का उल्लेख हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 15 और धारा 16 में किया गया है। एक हिंदू महिला की निर्वसीयत उत्तराधिकार इस अधिनियम की धारा 15 द्वारा शासित होती है, जब वह बिना वसीयत छोड़े मर जाती है। हिंदू महिला के कानूनी उत्तराधिकारियों के शेयरों का निर्धारण करने से पहले, सही उत्तराधिकार प्रावधानों को लागू करने के लिए संपत्ति की उत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। यदि किसी हिंदू महिला को संपत्ति विरासत में मिलती है और उसके जीवित बच्चे या पोते-पोतियां हैं, तो अधिनियम की धारा 15(1) लागू होगी। हालाँकि, यदि कोई जीवित बच्चे या पोते-पोतियाँ नहीं हैं, तो धारा 15(2) लागू होती है। स्व-अर्जित संपत्ति, वसीयत, उपहार, स्त्रीधन या अन्य माध्यम से प्राप्त संपत्ति के लिए धारा 15(1) लागू होती है।
हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
परिचय
हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 बच्चों के कल्याण पर जोर देते हुए अल्पवयस्कता और संरक्षकता से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समेकित करता है। यह अधिनियम 25 अगस्त, 1956 को अधिनियमित किया गया था, और अवयस्कों की समृद्धि को प्राथमिकता देते हुए, हिंदू समुदाय के भीतर अल्पवयस्कताों और संरक्षकता से संबंधित कानूनों को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस अधिनियम में 13 धाराएं शामिल हैं जो न केवल अल्पवयस्कता और संरक्षकता के सिद्धांतों से संबंधित हैं बल्कि किसी व्यक्ति की बच्चे के संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए आवश्यक शक्तियों और प्रकारों और योग्यताओं पर भी प्रकाश डालती हैं
अधिनियम का अनुप्रयोग
अधिनियम की धारा 3 क़ानून के अनुप्रयोग को बताती है। यह धारा हिंदुओं पर लागू होती है, जिनकी व्याख्या ऐसे व्यक्तियों के रूप में की जाती है जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, या वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज को मानते हैं। अधिनियम आगे बौद्धों, सिखों और जैनियों को अधिनियम के अनुप्रयोग के लिए पात्र बनाता है और उन्हें हिंदू माना जाता है, जैसा कि धारा 3(1)(b) के तहत कहा गया है। अधिनियम यह भी निर्दिष्ट करता है कि यह किस पर लागू नहीं होता है, जिसमें धर्म के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी शामिल हैं, जिसका उल्लेख धारा 3(1)(c) के तहत किया गया है।
यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अर्थ के भीतर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अपवाद निर्धारित करता है, जिसमें कहा गया है कि यह क़ानून जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं है।
प्राकृतिक संरक्षक
हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्दिष्ट हैं, जहां एक अविवाहित लड़की, एक लड़के, एक नाजायज अविवाहित लड़की या एक लड़के के प्राकृतिक संरक्षक निर्दिष्ट हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि अधिनियम की धारा 6(c) के तहत एक पति एक विवाहित महिला का संरक्षक होगा।
अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, दत्तक ग्रहण किए गए अवयस्क बच्चे का दत्तक पिता और दत्तक मां उसके प्राकृतिक संरक्षक होंगे।
प्राकृतिक संरक्षकों की शक्तियों का उल्लेख धारा 8 के तहत किया गया है, जहां यह निर्दिष्ट किया गया है कि, अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण के लिए अधिकृत होने के बाद भी, प्राकृतिक संरक्षकों को कुछ अधिकार, शक्तियां और प्रतिबंध दिए गए हैं। एक प्राकृतिक संरक्षक ऐसे कार्य करने की सारी शक्ति प्राप्त कर लेता है जिससे अवयस्क बच्चे को फायदा हो, साथ ही उसकी संपत्ति की सुरक्षा भी हो। अधिनियम की धारा 8(2) के तहत यह दावा किया गया है कि एक प्राकृतिक संरक्षक अदालत से पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी माध्यम से अवयस्क की संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है, और धारा 8(2)(b) के तहत अवयस्कों की किसी भी संपत्ति को पट्टे पर देने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 किसी प्राकृतिक संरक्षक की पूर्व अनुमति या ऐसे व्यक्तियों की अपील के मामले में लागू होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार एक अवयस्क, किसी अवयस्क के संरक्षक के रूप में कार्य करने में अक्षम है।
यह अधिनियम धारा 9 के तहत प्राकृतिक संरक्षकों के वसीयती अधिकारों को भी निर्धारित करता है। धारा निर्दिष्ट करती है कि प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले पिता या माता की मृत्यु के मामले में, वे एक वसीयत बनाने के लिए अधिकृत हैं, अवयस्क और उसकी संपत्तियाँ के संबंध में एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है। यह धारा 9(6) के तहत आगे निर्दिष्ट करता है, कि नियुक्त संरक्षकता अवयस्क लड़की की शादी के कारण समाप्त हो जाएगी।
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956, कानून के महत्वपूर्ण समूहों में से एक है जो हिंदू समुदाय के भीतर दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण की जटिलताओं पर केंद्रित है। यह अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है, जिसमें ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज परंपराओं का पालन करने वालों के साथ-साथ बौद्ध, सिख और जैन भी शामिल हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म जैसे अन्य प्रमुख धर्मों के कानूनों द्वारा शासित नहीं हैं। अधिनियम दत्तक ग्रहण के मानदंडों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें कहा गया है कि बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए और पहले दत्तक ग्रहण नहीं लिया गया होना चाहिए। अन्य विभिन्न मानदंड, पात्रता और योग्यताएं नीचे संक्षेप में उल्लिखित हैं।-

अधिनियम का अनुप्रयोग
अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, इस क़ानून के प्रावधान उन लोगों पर लागू हो सकते हैं जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज को मानते हैं। यह अधिनियम उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है, न कि उस व्यक्ति पर जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी है।
इस अधिनियम की धारा 2(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अर्थ के भीतर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अपवाद निर्धारित करती है, जिसमें कहा गया है कि यह क़ानून जनजाति के व्यक्तियों पर लागू नहीं है।
किसे दत्तक ग्रहण किया जा सकता है?
अधिनियम की धारा 10 उस व्यक्ति के मानदंड बताती है जो दत्तक ग्रहण के योग्य है। इसमें दावा किया गया है कि कोई व्यक्ति इस क़ानून के प्रावधानों के तहत दत्तक ग्रहण किए जाने के योग्य तभी है जब वह व्यक्ति धर्म से हिंदू है, पहले दत्तक ग्रहण नहीं लिया गया है, विवाहित नहीं है (जब तक कि कोई रीति रिवाज या प्रथा विवाहित होने पर दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं देता है), पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली (जब तक कि कोई रीति रिवाज या प्रथा पंद्रह वर्ष की आयु पूरी होने पर दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं देता है)।
वैध दत्तक ग्रहण
दत्तक ग्रहण के वैध होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जो अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारित हैं। इसमें व्यक्ति की दत्तक ग्रहण की क्षमता और अधिकार शामिल है, दत्तक ग्रहण किए जाने वाले व्यक्ति के पास दत्तक ग्रहण की क्षमता होनी चाहिए, और दत्तक ग्रहण वाला व्यक्ति दत्तक ग्रहण के लिए दिए गए व्यक्ति का संरक्षक या माता-पिता होना चाहिए।
वैध दत्तक ग्रहण की कुछ अन्य शर्तें
अधिनियम में दत्तक ग्रहण को वैध बनाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। धारा 11 ऐसी पूर्वापेक्षाओं को रेखांकित करती है, जो इस प्रकार हैं।-
- धारा 11(i) के अनुसार, बेटे को दत्तक ग्रहण के मामले में, दत्तक ग्रहण वाले व्यक्ति के पास दत्तक ग्रहण के समय कोई मौजूदा हिंदू बेटा, पोता या परपोता नहीं होना चाहिए।
- धारा 11(ii) के अनुसार, बेटी को दत्तक ग्रहण के मामले में, दत्तक ग्रहण वाले व्यक्ति के पास मौजूदा हिंदू बेटी, पोती या परपोती नहीं होनी चाहिए।
- धारा 11(iii) में कहा गया है कि यदि कोई पुरुष किसी कन्या को दत्तक ग्रहण ले रहा है, तो उसे दत्तक पुत्री से इक्कीस वर्ष बड़ा होना चाहिए।
- धारा 11(iv) में कहा गया है कि यदि कोई महिला किसी लड़के को दत्तक ग्रहण ले रही है, तो उसे दत्तक ग्रहण लिए गए लड़के से इक्कीस वर्ष बड़ी होनी चाहिए।
- एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ दत्तक ग्रहण नहीं लिया जा सकता है, जैसा कि धारा 11(v) के तहत उल्लिखित है।
- किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण देते समय उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा उचित और औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, और जिस व्यक्ति को दत्तक ग्रहण किया जा रहा है उसे उसके दत्तक माता-पिता द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख धारा 11(vi) के अंतर्गत किया गया है।
कौन किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए दे सकता है?
धारा 9(1) में कहा गया है कि केवल माता या पिता या संरक्षक ही बच्चे को दत्तक ग्रहण देने की क्षमता रखते हैं। हालाँकि, यह भी उल्लेख किया गया है कि, माता और पिता दोनों को अपने बच्चे को दत्तक ग्रहण देने में समान अधिकार होंगे, बशर्ते, उन्हें ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए।
बच्चे को दत्तक ग्रहण वाले व्यक्ति को वैध दत्तक ग्रहण की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसा कि धारा 6, धारा 7 और धारा 8 के तहत प्रदान किया गया है।
भारतीय संविधान में हिंदू कानून का अस्तित्व
भारतीय संविधान में हिंदू धर्म को शामिल करना इसके अनुच्छेदों में निहित समानता और स्वतंत्रता के प्रमुख सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, जो समानता के अधिकार के दायरे में आता है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करता है। धर्म के प्रति भेदभाव के कारण हिंदू कानून का इससे गहरा संबंध है, जो हिंदू धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों को भी स्वतंत्रता देता है। इसी तरह, अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार के बारे में कहता है जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बताता है। साथ में, ये संवैधानिक प्रावधान भारत में धार्मिक समानता और स्वतंत्रता के व्यापक ढांचे के भीतर हिंदू धर्म की उपस्थिति, मान्यता और सुरक्षा की पुष्टि करते हैं।
भारत के संविधान ने अपनी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को रेखांकित किया है और भारत के लोगों को इस सिद्धांत का पालन करने का आदेश दिया है। बयालीसवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 में ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द डाला गया, जिसे भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक माना जाता है। यह केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में फैसले के आधार पर स्थापित किया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले ने एक धर्म की प्रथा, व्याख्या और अभ्यास को प्रमाणित किया है, जिससे किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म और उसकी प्रथाओं को स्वीकार करने की अनुमति मिल गई है।
भारतीय संविधान हिंदू कानून की परंपराओं और प्रथा के दायरे को बढ़ाता है, जबकि इसके प्रथागत कानूनों को भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित करने की अनुमति देता है। हिंदू कानून की पारंपरिक कानूनी प्रणाली उन रीति रिवाजओं की परिकल्पना करती है जो क्षेत्रीय-केंद्रित या जाति-केंद्रित हो सकती हैं। भारतीय संविधान अपनी बुनियादी विशेषताओं में से एक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से मुक्ति के साथ ऐसी प्रथा की अनुमति देता है।
न्यायपालिका की भूमिका
भारतीय न्यायपालिका ने भारतीय प्रथागत कानूनों, विशेष रूप से हिंदू कानून की संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से, भारतीय न्यायपालिका ने व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को मजबूत किया है। इसने सामाजिक-कानूनी मामलों से संबंधित विभिन्न कानूनी मुद्दों को संबोधित करते हुए विभिन्न संवैधानिक पहलुओं की व्याख्या की है। निम्नलिखित ऐसे मामले हैं जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया और हिंदू कानून के विभिन्न आयामों को प्रभावित करते हुए ठोस कानूनी मिसाल कायम की।
सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)
तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ता सरला मुद्गल ने याचिका दायर कर दावा किया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसने दावा किया कि उसके पति ने इस्लाम अपना लिया और बहुविवाह की प्रथा का फायदा उठाया। उसने संतोष जताया कि ऐसी शादी शुरू से ही शून्य है और उसके पति ने द्विविवाह का अपराध किया है। इस मामले ने पारंपरिक रीति रिवाजओं का लाभ उठाने के लिए धार्मिक रूपांतरण के दुरुपयोग को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने पति की अपील को खारिज करते हुए दूसरी शादी को अवैध करार दिया। इसने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदू कानून के तहत संपन्न विवाह केवल अदालत के आदेश से ही समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, अदालत ने पत्नी द्वारा अपने और अपनी बेटी के लिए भरण-पोषण की मांग की गई डिक्री को बरकरार रखा।

जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)
तथ्य
इस मामले में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (भारतीय न्याय संहिता, 2023 में व्यभिचार को अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसे इस मामले द्वारा अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था) इस मामले में की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण प्रकृति का है क्योंकि यह एक महिला को उस महिला पर मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं देता है जिसके साथ उसके पति ने व्यभिचार किया है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि यह प्रावधान लैंगिक समानता का उल्लंघन है और महिलाओं की गरिमा को कमजोर करते हुए रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है।
निर्णय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बहुमत से ‘व्यभिचार’ को अपराध की श्रेणी से हटा दिया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत आता है। पीठ में पांच न्यायाधीश थे, जिनकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने की, जिन्होंने लैंगिक समानता, वैवाहिक रिश्ते में एक महिला की गरिमा और उसकी गरिमा से संबंधित संवैधानिक सिद्धांतों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। अदालत ने माना कि प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत असंवैधानिक था और लिंग-पूर्वाग्रह पर आधारित था।
अदालत ने आगे कहा कि यह प्रावधान प्रकृति में अतार्किक और सामंती (फ्यूडल) है और इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विवाह से बाहर के व्यक्तियों को दंडित करता है और पत्नी को अपने पति के खिलाफ मुकदमा दायर करने का अवसर प्रदान नहीं करता है।
रमेश चन्द्र रामप्रतापजी डागा बनाम रामेश्वरी रमेश चंद्र डागा (2005)
तथ्य
इस मामले में, पत्नी को अपनी दूसरी शादी में रहते हुए अपने दूसरे पति से घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा। इसके बाद पत्नी अपनी बेटी के साथ ससुराल छोड़कर अलग रहने लगी। हालाँकि, पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि माहेश्वरी लोगों के समूह द्वारा अपनाए जाने वाले प्रथागत नियमों में से एक के अनुसार की गई थी, जिसे ‘चोर चिट्ठी’ के नाम से जाना जाता है।
उसने न्यायिक अलगाव की प्रार्थना की और अपने और अपनी बेटी के लिए भरण-पोषण का दावा किया। उसके दूसरे पति ने दावों से बचने के लिए तर्क दिया कि उसकी पत्नी की पहली शादी ठीक से भंग नहीं हुई थी, इसलिए हिंदू कानून के तहत उनकी मौजूदा शादी अमान्य हो गई।
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह केवल हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत निर्धारित प्रावधानों के आधार पर ही भंग किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(i) का उल्लंघन किया गया था और ‘चोर चिट्ठी’ जैसी रीति रिवाज को कानून की नजर में मान्यता नहीं दी गई थी।
पत्नी द्वारा अपने और अपनी बेटी के लिए की गई अपील के संबंध में, अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 25 के संबंध में स्थायी भरण-पोषण की अनुमति दे दी। इसने प्रावधान की व्यापक रूप से व्याख्या की, जिसमें अमान्यता के आदेश सहित भरण-पोषण देना शामिल था। अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर जोर दिया और माना कि पत्नी को अपने और अपनी बेटी के लिए दावा किया गया भरण-पोषण मिलना चाहिए, भले ही पहली शादी कभी भी कानूनी रूप से भंग नहीं हुई, जिससे उसकी दूसरी शादी रद्द हो गई।
सुशील कुमारी डांग बनाम प्रेम कुमार डांग (1976)
तथ्य
इस मामले में पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के उन्हें और उनके समाज को छोड़ दिया। इसके अलावा, पत्नी ने तर्क दिया कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और वह क्रूरता का शिकार हुई जहां उसके पति ने शराब पीकर घर आने के बाद उस पर शारीरिक हमला किया।
दिल्ली जिले की विचारण न्यायालय ने पति के दावों का समर्थन किया और वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश दिया। इसके बाद, पति ने अपनी पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए न्यायिक अलगाव की प्रार्थना की, जिसके खिलाफ उसकी पत्नी ने अपील की।
निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार नहीं रखा और इसे पलट दिया। अदालत ने पाया कि पति में अपनी पत्नी के साथ मेल-मिलाप करने के ईमानदार इरादे की कमी थी, यह देखते हुए कि पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री प्राप्त करने के तुरंत बाद न्यायिक डिक्री के लिए प्रार्थना की। अदालत ने आगे कहा कि यह सिर्फ अपनी पत्नी को परेशान करने के लिए था, और पति ने दोनों मुकदमे एक साथ दायर किए, जो कि अगर अनुमति दी गई तो कानून में बुरा होगा।
लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006)
तथ्य
इस मामले में, लता नाम की एक लड़की अपने भाई के साथ रहती थी, जहाँ से वह भ्रमा नंद गुप्ता से शादी करने के लिए भाग गई, जो उसकी जाति का नहीं था। काफी देर तक नहीं मिलने पर उसके भाई ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिससे लड़के के माता-पिता का पता चला। पता चलने पर, भाई ने अपनी बहन के पति के परिवार को धमकाना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया और अलग-अलग जातियों से होने के बावजूद भी उनकी शादी के प्रति तिरस्कार दिखाया।
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को अपनी जाति से बाहर शादी करने की आजादी है। आगे यह राय दी गई कि यदि उनके संबंधित माता-पिता इस तरह की शादी का विरोध करते हैं, तो वे धमकी देने, जबरदस्ती करने या सम्मान रक्षा हेतु हत्या करने के बजाय अपने बच्चों के साथ सामाजिक संपर्क तोड़ सकते हैं। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अंतर-जातीय जोड़ों के प्रति प्रोत्साहित अत्याचार को रोका जाना चाहिए और पुलिस को जांच रखने के लिए बाध्य किया गया।

सीमा बनाम अश्वनी कुमार (2006)
तथ्य
इस मामले में याचिकाकर्ता सीमा ने अपने पति अश्वनी कुमार के खिलाफ उनके बीच चल रहे विवाद को लेकर मामला दायर किया था। मामला अपील में चला गया और उच्चतम न्यायालय में चला गया, जिसने अपंजीकृत विवाहों से संबंधित एक व्यापक मुद्दे पर गौर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर राय जानने के लिए कई राज्यों को नोटिस जारी किया।
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तियों के सामाजिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया। यह भी देखा गया कि इस तरह के रिकॉर्ड विवाह और उससे जुड़े मुद्दों पर विवादों के समय मददगार साबित हो सकते हैं। अदालत ने तीन महीने के भीतर विवाह के पंजीकरण और नियुक्ति अधिकारियों को अनिवार्य करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसने उचित प्राधिकारियों को लागू करने और गैर-अनुपालन के लिए दंड लागू करने का भी आदेश दिया।
श्रीमती प्रफुल्ल बाला मुखर्जी बनाम सतीश चंद्र मुखर्जी और अन्य (1997)
तथ्य
इस मामले में, वादी-अपीलकर्ता ने दो मंजिला घर के स्वामित्व को स्थापित करने का दावा करते हुए एक घोषणा की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया। उन्होंने प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की। घर गोपाल मुखर्जी का है, जो वादी का भाई और प्रतिवादी का पिता है। हालाँकि, वादी ने यह दावा करते हुए उस घर के स्वामित्व का दावा किया कि उसने और उसके पति ने गणेश चंद्र मुखर्जी को दत्तक ग्रहण किया था, जो गोपाल मुखर्जी के पुत्रों में से एक थे। गणेश चंद्र मुखर्जी की मृत्यु के बाद, वादी ने दो मंजिला घर के स्वामित्व का दावा किया, जिसे प्रतिवादियों ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि दत्तक ग्रहण वैध नहीं था।
निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दत्तक ग्रहण को अवैध माना और वादी के सभी दावों को खारिज कर दिया। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से पता चलता है कि गणेश चंद्र मुखर्जी ने अपने जैविक माता-पिता को अपने माता-पिता के रूप में मानना जारी रखा है और उनके साथ संबंध बनाए रखा है, इसलिए वादी के अपनी दत्तक मां होने के दावे को खारिज कर दिया है। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि दत्तक ग्रहण से संबंधित आवश्यक समारोह पूरे नहीं किए गए, और कोई औपचारिकताएं निष्पादित नहीं की गईं।
एन जी दास्ताने बनाम एस दास्ताने (1975)
तथ्य
इस मामले में पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। अपने बचाव में, प्रतिवादी-पत्नी ने तर्क दिया कि इस तरह के दावे मनगढ़ंत थे और उसके पति के कार्यों और उसकी घोर उपेक्षा के कारण विवाह बिगड़ गया। कथित तौर पर पति ने पत्नी को मनोचिकित्सक से परामर्श लेने के लिए मजबूर किया लेकिन उसके इनकार के कारण वह असफल रहा। पत्नी ने आगे कहा कि उसकी ओर से क्रूरता की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और उसके पति के दावे और दलीलें सिर्फ उसे परेशान करने और शादी को खत्म करने के लिए थीं।
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय क्रूरता के आरोप की बारीकियों का आकलन करने में विफल रहा और प्रदान किए गए सबूतों से बताई गई तथ्यात्मक व्याख्या की उपेक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सबूतों पर आगे विचार करने के बाद बताया कि प्रतिवादी की ओर से ऐसा आचरण किया गया है जो क्रूरता के बराबर है। हालाँकि, अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता और परित्याग के दावों को प्रमाणित करना संभव नहीं था क्योंकि प्रतिवादी के पहले के कार्यों को अपीलकर्ता द्वारा माफ कर दिया गया था।
जीजाबाई बनाम पठानखान (1970)
तथ्य
यह मामला प्राकृतिक संरक्षकता की अवधारणा से संबंधित है और प्राकृतिक संरक्षक कौन है। यह मामला तब सामने आया जब एक अवयस्क ने वयस्क होने के बाद किरायेदार, जो इस मामले में प्रतिवादी भी है, का पट्टा समाप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया। जमीन का टुकड़ा अपीलकर्ता को उसके पिता द्वारा उपहार में दिया गया था। किरायेदारी के दौरान, अपीलकर्ता अवयस्क थी और अपीलकर्ता के पिता की अनुपस्थिति के कारण, पट्टे का रख रखाव उसकी माँ द्वारा किया गया था। पट्टे की वैधता पर सवाल उठाया गया था, क्योंकि इसका प्रबंधन अपीलकर्ता की माँ द्वारा किया जाता था, न कि उसके पिता द्वारा। यह तर्क दिया गया कि, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम के अनुसार, एक पिता एक बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है, न कि माँ।
निर्णय
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पट्टे की वैधता को बरकरार रखा, जिसे अपीलकर्ता की मां ने तब निष्पादित किया था, जब वह अवयस्क थी। जबकि पट्टे की वैधता विवाद में थी, मां द्वारा किए गए निष्पादन को देखते हुए, जो हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम के अनुसार प्राकृतिक संरक्षक नहीं है, अदालत ने वैधता की पुष्टि की और कहा कि ऐसी स्थिति में जहां पिता अपने नाबालिग बच्चे के मामलों में निष्क्रिय, लापरवाह या अनुपस्थित है, मां बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक है।
ऐसे सुधारों की जरूरत
हिंदू कानून, जैसा कि 1950 के दशक से अस्तित्व में है, में कुछ तर्कसंगत विचारधाराओं और सामाजिक प्रगति का अभाव था। हिंदू कानून में सुधार हिंदू प्रथागत कानून के लंबे प्रावधानों में छिपी कुछ विसंगतियों और अपर्याप्तताओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण थे, जिन्हें बाद में ऐतिहासिक न्यायिक मिसालों के माध्यम से उजागर किया गया था। ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से, विभिन्न समसामयिक (कंटेंपररी) मुद्दों को संबोधित किया गया, जैसे कि पूर्व पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी पर प्रतिबंध, महिलाओं की गरिमा पर पर्दा डालने वाली व्यभिचार की रीति रिवाज को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उनके अधिकारों और विकल्पों का सम्मान करना।
हिंदू कानून के तहत कई कानून अपनी समय-सीमा पार कर चुके हैं, जिससे आधुनिक समय में अराजकता पैदा हो गई है। इस प्रकार, एक नए और न्यायसंगत दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, इन परिवर्तनों पर कानून के माध्यम से या न्यायिक मिसालों के माध्यम से विचार करना अपरिहार्य है। न्यायपालिका विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षकता और उत्तराधिकार से संबंधित सामाजिक व्यवधान और दुविधाओं से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। न्यायपालिका ने भी अपने ज्ञान और न्यायसंगत दृष्टिकोण को समझने की प्रतिबद्धता के साथ, हिंदू प्रथागत कानूनों की व्याख्या करके भारतीय कानूनी प्रणाली को मुक्त कर दिया है।

निष्कर्ष
हिंदू कानून के कई रंग हैं और इसकी प्रकृति व्यापक है। हिंदू कानून के व्यापक क्षेत्र में कई अधिनियम शामिल हैं, जिनमें से कुछ पर लेख में संक्षेप में चर्चा की गई है। हिंदू कानून जैसे स्वीय कानून को नियंत्रित करने वाले कानूनों की शुरुआत के साथ, पारंपरिक अदालतों की दीवारों के भीतर स्वीय कानूनों का कामकाज आसान हो गया है। स्वीय कानून का संहिताकरण वास्तव में ऐतिहासिक है। यह सिर्फ कानून बनाना और लागू करना नहीं है, बल्कि धार्मिक भावनाओं, रीति-रिवाजों, प्रथाओं और बहुत कुछ को शामिल करना है।
इस प्रकार, हिंदू कानून का परिचय किसी किताब से कम नहीं होगा क्योंकि इसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, 1956, संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 और भी बहुत कुछ जैसे स्वीय कानूनों से संबंधित कई कानून शामिल हैं। यह लेख अत्यधिक विविध हिंदू कानून का एक विचार प्रदान करने का प्रयास करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या किसी महिला का स्त्रीधन किसी वैधानिक प्रावधान के तहत सुरक्षित है?
एक महिला का उसके स्त्रीधन का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के तहत सुरक्षित है, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 के साथ पढ़ा जाता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भले ही स्त्रीधन के तहत संपत्ति उसके पति या ससुराल वालों द्वारा कब्जा कर ली गई हो, वे केवल ऐसी संपत्ति के न्यासी (ट्रस्टी) हैं और उन्हें इसे इसके मालिक यानी पत्नी को वापस करना होगा। इसके अलावा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 18(e) स्त्रीधन को पत्नी के अधिकारों में से एक के रूप में मान्यता देती है और कहती है कि एक महिला को आभूषण, कपड़े, स्त्रीधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित अपनी संपत्ति वापस पाने का अधिकार है, और क़ानून उसके वित्तीय हितों की रक्षा के लिए ‘आर्थिक दुर्व्यवहार’ को भी संबोधित करता है।
क्या कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी हिंदू व्यक्ति से शादी कर सकता है?
हां, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत एक हिंदू और मुस्लिम व्यक्ति एक-दूसरे से शादी कर सकते हैं। उनके बीच का विवाह हिंदू स्वीय कानून के तहत शून्यकरणीय होगा और मुस्लिम स्वीय कानून के तहत अनियमित (फासीद) होगा।
क्या धर्म परिवर्तन से विवाह अस्वीकार हो जाता है?
नहीं, किसी भी पक्ष द्वारा विवाह में धर्म परिवर्तन करने पर विवाह विघटित नहीं होता है। हालाँकि, इस तरह के रूपांतरण पर, दूसरा पक्ष इस आधार पर तलाक के लिए अदालत के समक्ष याचिका दायर कर सकता है। यह धारा 13 विशिष्ट रूप से, धारा 13(1)(ii) के तहत उल्लिखित आधारों में से एक है।
क्या कोई अकेली महिला बच्चा का दत्तक ग्रहण कर सकती है?
हां, एक अविवाहित महिला किसी बच्चे का दत्तक ग्रहण ले सकती है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, बशर्ते कि उसे सक्षम होना होगा और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 6 और धारा 8 के तहत प्रावधानों का पालन करना होगा। हालाँकि, दत्तक ग्रहण को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा भी विनियमित किया जाता है, जो एक वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम की विनियम संख्या 5 दत्तक ग्रहण के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करती है। यह एक अविवाहित महिला को एक लड़की या लड़के को दत्तक ग्रहण के लिए पात्र बनाता है, जबकि एक अविवाहित पुरुष को केवल एक लड़के को दत्तक ग्रहण में सक्षम बनाता है।
संदर्भ
- Hindu Law and The Constitution, A.M Bhattacharjee, 2 ed. 1994.
- Modern Hindu Law by Paras Diwan.







