यह लेख Nikita Singh द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से इंटरनेशनल कॉन्ट्रेक्ट, नेगोसिएशन, ड्राफ्टिंग एंड एनफोर्समेंट में डिप्लोमा कर रही हैं। इस लेख मे रोजगार विवादों में एडीआर की भूमिका, एडीआर क्या है, रोजगार विवादों में प्रयुक्त एडीआर के तरीकों, उनसे संबंधित कानूनों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
आज की तेजी से बदलती दुनिया में, एडीआर एक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि लोगों के पास पारंपरिक मुकदमेबाजी प्रणाली जैसी लंबी समाधान प्रक्रिया के लिए समय या धैर्य नहीं है। इसके विपरीत, एडीआर को काफी लोकप्रियता मिली है, क्योंकि यह मुकदमेबाजी की तुलना में कम समय लेने वाला, सस्ता, गोपनीय और लचीला विकल्प है। रोजगार विवाद, जो लगभग अपरिहार्य हो गए हैं, उन्हें हल करने के लिए भी एडीआर का उपयोग किया जाता है। रोजगार विवाद कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कार्यस्थल पर उत्पीड़न, गैरकानूनी बर्खास्तगी, अनुबंध का उल्लंघन, या कोई अन्य विवाद। इन सभी मुद्दों का उत्पादकता और समग्र कार्यस्थल के माहौल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, और इन्हें शीघ्रतापूर्वक और गोपनीय तरीके से हल करने के लिए, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही एडीआर का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो, आखिर एडीआर क्या है और यह रोजगार विवादों को सुलझाने में कैसे मदद करता है?
एडीआर उन तकनीकों या विधियों के समूह को संदर्भित करता है जिनका उपयोग अदालत के बाहर विवादों या असहमतियों को हल करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक मुकदमेबाजी प्रणालियों की तुलना में, एडीआर एक सस्ती, लचीली, गोपनीय और कम समय लेने वाली प्रक्रिया है, जो इसे शीघ्र और लागत प्रभावी समाधान के लिए वांछनीय बनाती है। इस लेख में हम रोजगार विवादों में एडीआर की भूमिका, इसके तरीकों तथा प्रत्येक के फायदे और नुकसान पर चर्चा करेंगे।
वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) क्या है?
वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर), जिसे बाह्य विवाद समाधान के रूप में भी जाना जाता है, न्यायालय के बाहर विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों को संदर्भित करता है। यह पारंपरिक मुकदमेबाजी प्रणाली के विकल्प के रूप में कार्य करता है। इन तरीकों में आमतौर पर एक तीसरा पक्ष शामिल होता है, जो विवादों को निपटाने में मदद करता है। मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), सुलह (कन्सिलिएशन), बिचवई (मिडिएशन) और वार्ता (निगोशिएशन) एडीआर के सामान्य रूप हैं; वे मुकदमेबाजी के लिए लागत प्रभावी, तीव्र और लचीले विकल्प हैं। एडीआर विवाद समाधान का एक ऐसा तंत्र है जो गैर-विरोधात्मक है, अर्थात, सभी के लिए सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचने के लिए एक साथ मिलकर काम करना है। ये विधियाँ व्यक्तियों को विवादों को सुलझाने तथा पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुँचने में सहायता करती हैं। इनमें से प्रत्येक विधि एक विशिष्ट तरीके से समझौता करने में सहायक होती है, जिसके लाभ और नुकसान विवाद की प्रकृति और इसमें शामिल लोगों पर निर्भर करते हैं।

रोजगार विवादों में प्रयुक्त एडीआर के तरीके
मध्यस्थता
मध्यस्थता रोजगार विवादों में प्रयुक्त एडीआर के सबसे सामान्य रूपों में से एक है। रोजगार समझौते में आमतौर पर एक मध्यस्थता खंड शामिल होता है, जो विवादों का समाधान मुकदमेबाजी के बजाय मध्यस्थता के माध्यम से करने का अधिकार देता है। मध्यस्थता में, पक्ष एक तटस्थ तीसरे पक्ष की नियुक्ति करते हैं, जिसे मध्यस्थ या मध्यस्थों के पैनल के रूप में जाना जाता है, और वे मध्यस्थयों के निर्णय का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। मध्यस्थ अपने क्षेत्र या जिस विवाद को वे सुलझा रहे हैं, उसके विषय-वस्तु के विशेषज्ञ होते हैं, तथा मामले में ज्ञानवर्धक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मध्यस्थ दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है, उनके साक्ष्यों की जांच करता है और उसके आधार पर अपना निर्णय सुनाता है। मध्यस्थ के निर्णयों को मध्यस्थीय पंचाट कहा जाता है, और वे दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।
मध्यस्थता का उपयोग करने के लाभ
गोपनीय
मध्यस्थता भी एक गोपनीय प्रक्रिया है। पक्षकार कई कारणों से अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता को चुनते हैं, जिनमें से एक कारण यह है कि यह एक निजी और गोपनीय प्रक्रिया है। मानक न्यायालय प्रणाली सभी के लिए खुली है, लेकिन मध्यस्थता चीजों को निजी रखती है। मध्यस्थता की गोपनीय व्यवस्था में पक्ष संवेदनशील जानकारी और विवाद विवरण को निजी रख सकते हैं।
तेज़ समाधान
पारंपरिक मुकदमा प्रणाली एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है; इसे पूरी तरह से हल होने में महीनों या वर्षों तक का समय लग सकता है। इसके विपरीत, मध्यस्थता एक छोटी और कम समय लेने वाली प्रक्रिया है जो विवादों या असहमतियों को कुछ दिनों या हफ्तों में सुलझा देती है।
प्रभावी लागत
मध्यस्थता का एक अन्य लाभ यह है कि यह लागत प्रभावी है, अर्थात यह पारंपरिक मुकदमा प्रणालियों की तुलना में बहुत सस्ता है। पारंपरिक मुकदमेबाजी प्रक्रिया कठोर होती है और लंबी अवधि तक चलती है तथा इसमें न्यायालय शुल्क, वकील शुल्क और अन्य शुल्क-संबंधी भुगतान जैसे निरंतर भुगतान शामिल होते हैं। चूंकि मध्यस्थता लंबे समय तक नहीं चलती और जल्दी ही निपट जाती है, इसलिए इसमें कम धनराशि की आवश्यकता होती है।
विशेषज्ञता
मध्यस्थ अपने क्षेत्र या विवाद के विषय-वस्तु के विशेषज्ञ होते हैं, जो मामले में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। विवादों को सुलझाते समय सुविचारित और सटीक निर्णय लेने के लिए विषय-वस्तु की गहन समझ होना महत्वपूर्ण है।
मध्यस्थता का उपयोग करने के नुकसान
मिसाल का अभाव
मध्यस्थता का एक प्रमुख दोष कानूनी मिसाल का अभाव है। न्यायालय के निर्णयों के विपरीत, मध्यस्थता निर्णय भविष्य के मामलों के लिए कानूनी मिसाल कायम नहीं करते हैं। चूंकि मध्यस्थ स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय देते हैं, इसलिए निर्णय पर विचार किए बिना समान विवादों को हल करते समय असंगतियां उत्पन्न होना संभव है।
सीमित उपचार
पारंपरिक मुकदमेबाजी की तुलना में मध्यस्थता सीमित उपचार प्रदान करती है। मध्यस्थता उपलब्ध उपचारों या राहत के प्रकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, जिससे व्यापक मुआवजा या न्यायसंगत राहत, जैसे कि निषेधाज्ञा या विशिष्ट निष्पादन, प्राप्त करने की क्षमता सीमित हो सकती है। यह सीमा विशेष रूप से जटिल विवादों में नुकसानदेह हो सकती है, जिनमें अधिक व्यापक या गैर-मौद्रिक राहत की आवश्यकता होती है।
महंगा पड़ सकता है
लोग प्रायः मध्यस्थता को मुकदमेबाजी के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में देखते हैं, लेकिन कभी-कभी यह महंगा भी हो सकता है। मध्यस्थता व्यय में न केवल मध्यस्थ शुल्क शामिल है, बल्कि मध्यस्थता संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रशासनिक शुल्क और कानूनी प्रतिनिधित्व शुल्क भी शामिल हैं। ये खर्च उन व्यक्तियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं जो पहले से ही वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
अपील के लिए सीमित आधार
मध्यस्थता के निर्णय आमतौर पर अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, तथा अपील के लिए आधार बहुत सीमित होते हैं। आमतौर पर, केवल मध्यस्थ के कदाचार या प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण ही मध्यस्थता पंचाट (अवॉर्ड) से असंतुष्ट पक्षकारों को निर्णय को चुनौती देने का अवसर मिलता है। अपील की यह सीमित गुंजाइश समस्यामूलक हो सकती है यदि कोई पक्ष यह मानता है कि मध्यस्थ का निर्णय अनुचित या गलत था।
सुलह
सुलह भी रोजगार संबंधी विवादों को अदालत के बाहर निपटाने का एक तरीका है। पक्षकार अपने विवादों की सुनवाई और निर्णय के लिए एक मध्यस्थ, एक तटस्थ तीसरे पक्ष की नियुक्ति करते हैं। मध्यस्थ का मुख्य कार्य पक्षों को सौहार्दपूर्ण समझौते तक पहुंचने में सहायता करना है। मध्यस्थता के विपरीत, जहां मध्यस्थ का निर्णय पक्षों को बाध्य करता है, सुलह पक्षों को मध्यस्थ के निर्णय से अप्रभावित रहने की अनुमति देता है। यदि वे निर्णय से असंतुष्ट होंगे तो वे उसे अस्वीकार कर सकते हैं। यदि वे सहमत हों, तो मध्यस्थ उन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता या करार बनाने में सहायता कर सकता है।

सुलह-समझौता के लाभ
गोपनीय
सुलह एक निजी और गोपनीय प्रक्रिया है। अदालती प्रक्रियाओं के विपरीत, जो सार्वजनिक होती हैं और पक्षों के बारे में संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर सकती हैं, सुलह एक निजी व्यवस्था में होती है। इसका अर्थ यह है कि सुलह प्रक्रिया के दौरान कही गई हर बात गुप्त रहती है, जिससे पक्षकार अपने मतभेदों को निजी रख सकते हैं और सार्वजनिक नजरों से दूर रख सकते हैं।
सहयोग में वृद्धि
सुलह से पक्षों को प्रतिस्पर्धात्मकता के बजाय सहयोगात्मक रूप से काम करने की अनुमति मिलती है। पक्षकार प्रभावी ढंग से विवादों को सुलझा सकते हैं तथा सुलह-समझौते के माध्यम से अपने संबंधों को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आगे और अधिक नुकसान को रोका जा सकता है। इन रिश्तों को बरकरार रखने से भविष्य में साथ मिलकर काम करने और एक-दूसरे की मदद करने के अवसर मिल सकते हैं।
परिणाम पर नियंत्रण
सुलह-समझौता विवादों के परिणाम को नियंत्रित करने का लाभ प्रदान करता है, जबकि पारंपरिक न्यायालय प्रणाली में न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। सुलह में, मध्यस्थ पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने में सहायता करता है, लेकिन कोई निर्णय नहीं थोपता है; पक्ष प्रस्तावित समाधान को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
तेज़ समाधान
त्वरित समाधान सुलह का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। पारंपरिक मुकदमा प्रणाली एक लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है; इसे पूरी तरह से हल होने में महीनों या वर्षों तक का समय लग सकता है। दूसरी ओर, सुलह एक संक्षिप्त और कम समय लेने वाली प्रक्रिया है जो विवादों या असहमतियों को कुछ ही दिनों या हफ्तों में सुलझा देती है।
सुलह का उपयोग करने के नुकसान
शक्ति का असंतुलन
रोजगार संबंधी विवादों में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच महत्वपूर्ण शक्ति असंतुलन हो सकता है। सुलह इस असंतुलन को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मध्यस्थ की भूमिका किसी भी पक्ष की वकालत करने के बजाय केवल संचार को सुविधाजनक बनाना है। इससे अधिक शक्तिशाली पक्ष के पक्ष में परिणाम निकल सकते हैं, विशेष रूप से यदि मध्यस्थ शक्ति असंतुलन को प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं करता है।
गैर-बाध्यकारी प्रकृति
सुलह-समझौते का एक और दोष यह है कि इसका परिणाम बाध्यकारी नहीं होता। सुलह में, पक्षकार सुलहकर्ता के निर्णय या सुझाव से बाध्य नहीं होते हैं; यदि पक्षकार इससे संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें समाधान को अस्वीकार करने का अधिकार होता है। इस प्रकार, सुलह के माध्यम से प्राप्त कोई भी समझौता तब तक कानूनी रूप से लागू नहीं होता जब तक कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से उसका पालन न करें।
सुलहकार का सीमित अधिकार
सुलह में एक मध्यस्थ शामिल होता है जो पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने में मदद करता है। न्यायाधीश या मध्यस्थ के विपरीत, सुलहकार के पास निर्णयों को लागू करने या परिणाम थोपने का अधिकार नहीं होता है। यदि सुलहकार के प्रयासों से समझौता नहीं होता है, तो पक्षों को अन्य ए.डी.आर. प्रक्रियाओं या मुकदमेबाजी की ओर बढ़ना पड़ सकता है, जिससे विवाद को सुलझाने में लगने वाली समय-सीमा बढ़ सकती है और लागत भी बढ़ सकती है।
समाधान की कोई गारंटी नहीं
सुलह का उद्देश्य पक्षों को एक समान आधार खोजने तथा एक सुलहकार की सहायता से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो मतभेदों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। हालांकि, यदि सुलह से कोई समझौता नहीं होता है, तो पक्षों को विवाद को अधिक औपचारिक एडीआर प्रक्रियाओं या मुकदमेबाजी तक बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे मामले को सुलझाने में अतिरिक्त देरी और खर्च होने की संभावना हो सकती है।
बिचवई
बिचवई भी एडीआर की विधियों में से एक है। यह कम औपचारिक और अधिक लचीली विधि है। एक तटस्थ (न्यूट्रल) तृतीय पक्ष, जिसे बीच-बचावकर्ता कहा जाता है, पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है। बीच-बचावकर्ता कोई निर्णय नहीं देता; वह पक्षों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। बीच-बचावकर्ता का उद्देश्य दोनों पक्षों के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जीत वाला परिणाम प्राप्त करना है। यदि बिचवई के दौरान पक्षकारों के बीच समझौता हो जाता है, तो बीच-बचावकर्ता औपचारिक समझौता लिखने में मदद कर सकता है। यह समझौता आम तौर पर स्वैच्छिक होता है और दोनों पक्षों की आपसी सहमति को दर्शाता है।
बिचवई के लाभ
किफायती और तेज़ समाधान
बिचवई एक सस्ती एवं त्वरित समाधान प्रक्रिया है। मुकदमेबाजी के विपरीत, जो महीनों या वर्षों तक चल सकती है, जिसके कारण अंततः उससे जुड़ी महत्वपूर्ण कानूनी शुल्क भी बढ़ जाता है, बिचवई विवादों को कुछ दिनों या हफ्तों में सुलझा देती है, तथा किफायती और त्वरित समाधान प्रदान करती है।
लचीला
बिचवई एडीआर की कम कठोर तथा अधिक लचीली विधि है। बिचवई पक्षों को बैठक के लिए किसी भी स्थान और समय का चयन करने की लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करती है, साथ ही प्रक्रिया को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने की भी अनुमति देती है। यह लचीलापन विभिन्न प्रकार की प्राथमिकताओं और परिस्थितियों को समायोजित करके बिचवई प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाता है।
सहयोग में वृद्धि
बिचवई में, पक्षकार पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए बीच बचावकर्ता के साथ सक्रिय भागीदारी करते हैं। बिचवई शत्रुतापूर्ण वातावरण के बजाय सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करती है। यह सहयोगात्मक वातावरण पक्षों के बीच संबंधों को बनाए रखते हुए वांछित समाधान तक पहुंचने में सहायता करता है।
परिणाम पर नियंत्रण
बिचवई प्रक्रिया विवाद के परिणाम पर पर्याप्त नियंत्रण प्रदान करती है। पारंपरिक मुकदमेबाजी प्रणाली के विपरीत, जहां अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, बिचवई में पक्षकार स्वयं विवाद का परिणाम निर्धारित करते हैं, जबकि बीच बचावकर्ता केवल पक्षों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है और संभावित समाधान प्रदान करता है।
बिचवई के नुकसान
समाधान की कोई गारंटी नहीं
बिचवई विवाद के समाधान की गारंटी नहीं देती, क्योंकि यह एक गैर-बाध्यकारी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षों के स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी समाधान पर नहीं पहुंचते हैं, तो बीच-बचावकर्ता (मीडिएटर) की पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाती है, और उन्हें विवादों को सुलझाने के लिए एडीआर या मुकदमेबाजी की एक अलग पद्धति का विकल्प चुनना पड़ता है।
बीच बचावकर्ता के सीमित अधिकार
बिचवई में, मध्यस्थ की भूमिका पक्षों के बीच संचार और बातचीत को सुविधाजनक बनाना है ताकि उन्हें अपने समझौते तक पहुंचने में मदद मिल सके। बीच बचावकर्ता को निर्णय थोपने या बाध्यकारी निर्णय देने का अधिकार नहीं है। यदि बिचवई से कोई समाधान नहीं निकलता है, तो पक्षों को विवाद समाधान के अन्य तरीकों या मुकदमेबाजी पर विचार करना पड़ सकता है, जिससे समय और लागत बढ़ सकती है।
सीमित कानूनी संरक्षण
विवाद से जुड़े पक्षों को बिचवई में सीमित कानूनी संरक्षण प्राप्त है क्योंकि यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। यद्यपि अदालती कार्यवाही सख्त होती है, फिर भी वह पक्षकारों को सुरक्षा प्रदान करती है तथा उनके हितों की रक्षा करती है। बिचवई मुकदमेबाजी के समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हो सकती। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच शक्ति असंतुलन अक्सर रोजगार विवादों में कर्मचारी के हित को प्रभावित करता है।
गैर-बाध्यकारी प्रकृति
बिचवई का एक अन्य दोष यह है कि इसका परिणाम बाध्यकारी नहीं होता है। बिचवई में, बीच बचावकर्ता के पास अपने निर्णय थोपने का कोई अधिकार नहीं होता; इसके बजाय, वह पूरी तरह से पक्षों के स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार, बिचवई के माध्यम से प्राप्त कोई भी समझौता तब तक कानूनी रूप से लागू नहीं होता जब तक कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से उसका पालन न करें।
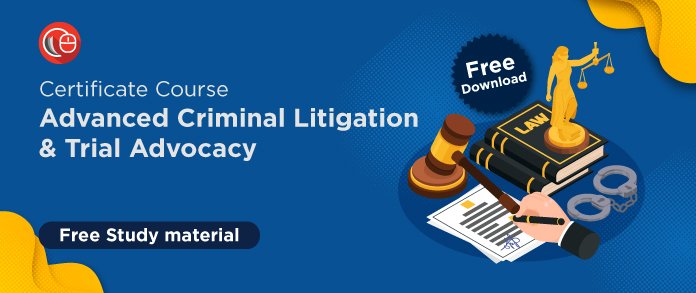
वार्ता
वार्ता से तात्पर्य पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए पक्षों के बीच संचार और चर्चा से है। विवादों को सुलझाने में यह लगभग हमेशा पहला कदम होता है, और इसमें पक्षों के बीच स्वैच्छिक संचार शामिल होता है; केवल तभी जब वार्ता विफल हो जाती है, तो पक्ष विवाद को सुलझाने के लिए कोई अन्य तकनीक अपनाते हैं। वार्ता में, पक्षकार स्वयं या किसी वार्ताकार की सहायता से, असहमति को दूर करने तथा पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए कई बार बातचीत करते हैं। वार्ता विवादों को सुलझाने का एक अनौपचारिक, सस्ता, लचीला और कुशल तरीका है। अदालती कार्यवाही की कठोर संरचना के विपरीत, वार्ता पक्षों को प्रत्यक्ष चर्चा के लिए आमने-सामने लाती है, जिससे उन्हें सभी की आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने का अवसर मिलता है।
वार्ता के लाभ
प्रभावी लागत
मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की तुलना में वार्ता बहुत सस्ता विकल्प है, क्योंकि इसमें कोई न्यायालय शुल्क या कानूनी प्रतिनिधि शुल्क शामिल नहीं होता है। चूंकि वार्ता एक अनौपचारिक प्रक्रिया है और इसे शीघ्रता से सुलझाया जा सकता है, इसलिए कुल व्यय आमतौर पर कम हो जाता है।
लचीला
वार्ता और कुछ नहीं बल्कि पक्षों के बीच चर्चा है; यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है, और पक्षों को बातचीत के समय, स्थान और यहां तक कि प्रक्रिया के संबंध में भी काफी लचीलापन प्रदान किया जाता है; सब कुछ पक्षों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं तय किया जाता है।
परिणाम पर नियंत्रण
वार्ता से पक्षों को अंतिम परिणाम पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त होता है। मुकदमेबाजी या मध्यस्थता के विपरीत, जहां प्राधिकरण का अंतिम निर्णय पक्षों पर बाध्यकारी होता है, वार्ता पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने की अनुमति देती है जो दोनों पक्षों के हितों को पूरा करता है।
सहयोग में वृद्धि
वार्ता पक्षों के बीच खुले संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के साथ-साथ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने में भी मदद कर सकता है।
वार्ता का उपयोग करने के नुकसान
विशेषज्ञता का अभाव
वार्ता में, पक्षकार स्वयं संचार और चर्चा की एक श्रृंखला के माध्यम से असहमति को हल करने का प्रयास करते हैं। यदि पक्षों में वार्ता में विशेषज्ञता का अभाव है, तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं और हितों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
भावनात्मक कारक
वार्ता के लिए दोनों पक्षों के बीच तार्किक और व्यावहारिक चर्चा की आवश्यकता होती है ताकि वे जीत वाली स्थिति पर पहुंच सकें। हालांकि, कभी-कभी पक्षों के व्यक्तिगत या भावनात्मक मुद्दे वार्ता के आड़े आ सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो जाती है।
समाधान के लिए औपचारिक तंत्र का अभाव
वार्ता पूरी तरह से पक्षों पर निर्भर करती है कि वे किसी समाधान पर पहुंचें और सहमत हों, जबकि मुकदमेबाजी या मध्यस्थता में प्राधिकारी निर्णय लेता है जो पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यदि पक्षकार किसी निर्णय पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो पूरी वार्ता प्रक्रिया बेकार हो जाएगी।
जटिल मुद्दों को संबोधित करने में कठिनाई
जटिल प्रकृति के विवादों में, वार्ता मुकदमेबाजी या मध्यस्थता जितनी प्रभावी या उपयोगी नहीं हो सकती है। जटिल विवादों के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है, जिसका पक्षों के पास अभाव हो सकता है। इससे समाधान प्रक्रिया रुक सकती है, और पक्ष को इस पर अधिक धन और समय खर्च करना पड़ सकता है।
रोजगार विवादों में एडीआर के लिए कानूनी ढांचा
एडीआर ने विवादों को कुशलतापूर्वक और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है; यह न केवल पक्षों को अदालत के बाहर विवादों को सुलझाने में सहायता करता है, बल्कि अदालत को न्यायिक बोझ से भी मुक्त करता है। विभिन्न क़ानूनों और न्यायिक उदाहरणों ने भारत में एडीआर के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया है।
सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी)
सीपीसी की धारा 89 एडीआर के माध्यम से अदालत के बाहर विवादों के निपटारे की बात करती है। सी.पी.सी. की धारा 89 में प्रावधान है कि:
जहां न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं, वहां न्यायालय समझौते की शर्तें तैयार करेगा तथा उन्हें पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए उपलब्ध कराएगा। पक्षों की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, न्यायालय संभावित समझौते की शर्तों को पुनः तैयार कर सकता है तथा समतुल्य (एक्विवलेंट) समझौते का संदर्भ दे सकता है। अदालत के बाहर समझौते के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:
- मध्यस्थता;
- सुलह
- न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से समझौता शामिल है; या
- बिचवई
जहां कोई विवाद संदर्भित किया जाता है-
- मध्यस्थता या सुलह के लिए, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता या सुलह के लिए कार्यवाही उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटान के लिए संदर्भित की गई थी;
- वहां न्यायालय उसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार लोक अदालत को संदर्भित करेगा और लोक अदालत को संदर्भित विवाद के संबंध में उस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे;
- न्यायिक निपटान के लिए, न्यायालय उसे उपयुक्त संस्था या व्यक्ति को संदर्भित करेगा और ऐसी संस्था या व्यक्ति को लोक अदालत माना जाएगा और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के सभी प्रावधान लागू होंगे मानो विवाद उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत लोक अदालत को संदर्भित किया गया हो;
- बिचवई के लिए, न्यायालय पक्षों के बीच समझौता कराएगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो निर्धारित की जा सकती है

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996
मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 भारत में मध्यस्थता और सुलह को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक न्यायिक प्रणाली से बाहर एक प्रभावी और कुशल विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है। इसका उद्देश्य पारंपरिक न्यायिक प्रणाली से बाहर एक प्रभावी और कुशल विवाद समाधान तंत्र प्रदान करना है। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक (कमर्शियल) मध्यस्थता पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) के मॉडल कानून पर आधारित है। अधिनियम मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों का अधिकार क्षेत्र और मध्यस्थता पंचाटो का प्रवर्तन शामिल है। इसमें सुलह को भी शामिल किया गया है तथा सुलह प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में रोजगार विवादों को नियंत्रित करता है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों/श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। यह रोजगार संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए ए.डी.आर. विधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। यह रोजगार संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और सुलह को प्रभावी तंत्र के रूप में मान्यता देता है। अधिनियम के अंतर्गत, सरकार नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों में मध्यस्थता के लिए सुलह अधिकारी या सुलह बोर्ड की नियुक्ति कर सकती है।
कानूनी मामले
किंगफिशर एयरलाइंस बनाम पृथ्वी मल्होत्रा एवं अन्य
यह मामला अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के विभिन्न स्टाफ सदस्यों द्वारा अवैतनिक वेतन और अन्य वेतन लाभों की वसूली के लिए शुरू की गई श्रम कार्यवाही से संबंधित था। जबकि कर्मचारियों ने विशेष रूप से सशक्त श्रम न्यायालयों में कार्यवाही शुरू की, किंगफिशर एयरलाइंस ने तर्क दिया कि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि रोजगार समझौते में मध्यस्थता खंड शामिल था। हालाँकि, किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और श्रम न्यायालय ने कार्यवाही पर अधिकार बरकरार रखा था।
मायावती ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रद्युत देब बर्मन
इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब पक्ष विवादों में मध्यस्थता के लिए सहमत होते हैं, तो अदालत की भूमिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6A) के तहत मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को निर्धारित करने तक सीमित होती है। न्यायालय को मध्यस्थ की नियुक्ति के दौरान विवाद के गुण-दोष की जांच नहीं करनी चाहिए।
एमआर कृष्ण मूर्ति बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि सरकार देश में बिचवई कार्यवाही को विनियमित करने के लिए भारतीय बिचवई अधिनियम बनाने पर विचार करे। न्यायालय ने मोटर दुर्घटना बिचवई प्राधिकरण की स्थापना के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने की भी सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को ऐसे विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता प्रकोष्ठ (सेल) बनाने का निर्देश दिया था।
कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से मोती राम (मृत) एवं अन्य बनाम अशोक कुमार एवं अन्य
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता की कार्यवाही स्वाभाविक रूप से निजी और गोपनीय होती है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मध्यस्थ को न्यायालय के समक्ष या तो सत्यापित समझौता प्रस्तुत करना चाहिए, यदि बिचवई सफल हो, अथवा यह कथन प्रस्तुत करना चाहिए कि बिचवई अप्रभावी थी।

निष्कर्ष
निष्कर्ष के तौर पर, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) रोजगार विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है, जो पारंपरिक मुकदमेबाजी प्रणाली की तुलना में अधिक सहयोगात्मक और कम विरोधाभासी दृष्टिकोण प्रदान करता है। मध्यस्थता, सुलह, बिचवई और वार्ता जैसे तरीकों को अपनाकर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही ऐसे समाधानों की दिशा में काम कर सकते हैं जो उनके व्यावसायिक संबंधों को सुरक्षित रखते हुए उनके हितों की रक्षा करें। एडीआर न केवल पक्षों का समय और पैसा बचाता है, बल्कि आवश्यकता और रुचि के अनुरूप परिणाम तैयार करने की लचीलापन भी प्रदान करता है। जैसे-जैसे कार्यस्थलों में परिवर्तन जारी रहेगा, रोजगार विवादों में एडीआर की भूमिका और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिससे ऐसे वातावरण को बढ़ावा मिलेगा जहां विवादों को निष्पक्षता और पारस्परिक सम्मान पर जोर देते हुए रचनात्मक तरीके से सुलझाया जाएगा।







