यह लेख लॉसिखो से एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, निगोशिएशन और विवाद समाधान में डिप्लोमा कर रही Tanvitha द्वारा लिखा गया है। इस लेख में दुर्व्यपदेशन (मिसरिप्रजेंटेशन), दुर्व्यपदेशन के प्रकार, माल की बिक्री के अनुबंध और उससे संबंधित कानूनी उपाय के बारे मे चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे आम लेन-देन चल वस्तुओं की खरीद और बिक्री है। माल बिक्री अधिनियम, 1930 चल माल की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करता है। ऐसे प्रयोजन के लिए किया गया कोई भी करार या अनुबंध माल की बिक्री अनुबंध के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। ऐसे अनुबंध में शामिल सबसे बड़ा जोखिम गलत बयानी है; यह अनुबंध के अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही हो जाता है। गलत बयानी से अनुबंध करने वाले पक्ष को कानून या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के ज़रिए नुकसानदेह अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सत्य के बारे में ऐसे झूठे बयान जानबूझकर या अनजाने में दिए जा सकते हैं। माल की बिक्री के अनुबंध में इस विशेष जोखिम की जांच करना महत्वपूर्ण है ताकि इसके निहितार्थ और उपलब्ध उपायों को समझा जा सके।
दुर्व्यपदेशन
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के तहत दुर्व्यपदेशन की परिभाषा दी गई है। अनुबंधों से संबंधित दुर्व्यपदेशन की अवधारणा को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया गया निर्दोष या जानबूझकर दिया गया झूठा बयान के रूप में परिभाषित किया गया है। दुर्व्यपदेशन किसी पक्ष को ऐसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है, जिसमें वह अन्यथा प्रवेश नहीं करता और इसके कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। बयान देने वाला पक्ष यह मान सकता है कि उसके शब्द सत्य हैं, ऐसी स्थिति में यह एक निर्दोष दुर्व्यपदेशन होगा, हालांकि यह जानबूझकर और कपटपूर्ण भी हो सकता है।
यह कब उत्पन्न होता है?

किसी अनुबंध के निर्माण से पहले बातचीत और चर्चा के चरण के दौरान दुर्व्यपदेशन उत्पन्न होती है। इस स्तर पर दिए गए कथन और दावे दूसरे पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रभावित करते हैं, इसलिए यह अनुबंध के निर्माण से पहले ही उत्पन्न हो जाता है। संविदा संबंधी चर्चा के प्रारंभिक चरण में अनुबंध से संबंधित तथ्यों के झूठे बयान और गलतियां की जाती हैं।
उदाहरण: X और Y, X की नाव को Y को बेचने पर चर्चा कर रहे हैं। X, Y को बताता है कि उसकी मोटर बोट 80 किमी/घंटा की गति तक जा सकती है; हालांकि, वह यह नहीं बताता कि उसने एक साल से अधिक समय से इसे नहीं चलाया है और उसका दावा केवल एक अनुमान है जिसकी शाब्दिक पुष्टि नहीं हुई है। Y नाव खरीदने के लिए सहमत हो जाता है और उसे पता चलता है कि मोटरबोट की गति केवल 50 किमी/घंटा है। यहाँ, X ने नाव की गति को गलत बताया और इस दुर्व्यपदेशन ने Y को इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया।
दुर्व्यपदेशन अनुबंध के उल्लंघन का आधार होगी और Y, X को उत्तरदायी ठहराते हुए अपने पास उपलब्ध उपचारों का प्रयोग कर सकता है।
दुर्व्यपदेशन के प्रकार
दुर्व्यपदेशन को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
निर्दोष दुर्व्यपदेशन
निर्दोष दुर्व्यपदेशन, इस ज्ञान के अभाव के कारण गलत तथ्यों का प्रस्तुतीकरण है कि कथन असत्य है।
निर्दोष दुर्व्यपदेशन का उपाय या तो अनुबंध को रद्द करना या निरसन करना है।
डेरी बनाम पीक मामला निर्दोष दुर्व्यपदेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहां प्रतिवादी के पास एक ट्रामवे कंपनी थी और वह वास्तव में मानता था कि स्टीम ट्राम के लिए अनुमोदन महज औपचारिकता मात्र थी, तथा कंपनी को अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अंततः अनुमति नहीं दी गई और कंपनी के शेयर खरीदने वाले वादी को नुकसान उठाना पड़ा। अदालत ने कहा कि कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उनका वास्तव में मानना था कि अनुमति एक औपचारिकता थी।
कपटपूर्ण दुर्व्यपदेशन
जब कोई प्रतिवादी कपटपूर्ण दुर्व्यपदेशन में संलग्न होता है, तो वह जानबूझकर किसी अन्य पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से झूठा बयान देता है। इस प्रकार का दुर्व्यपदेशन विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि इसमें धोखा देने और गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास किया जाता है। कपटपूर्ण दुर्व्यपदेशन को साबित करने के लिए, कई महत्वपूर्ण तत्वों को साबित किया जाना चाहिए। सबसे पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रतिवादी ने तथ्य का गलत बयान दिया है। यह कथन मौखिक या लिखित हो सकता है, और यह दूसरे पक्ष की निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, झूठा बयान दूसरे पक्ष को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण कारक रहा होगा। दूसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि प्रतिवादी को पता था कि बयान झूठा है या उसे इसकी सच्चाई या झूठ के प्रति कोई परवाह नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि या तो प्रतिवादी को पता था कि बयान झूठा है या फिर उसके पास इसे सच मानने का कोई उचित आधार नहीं था। तीसरा, यह दर्शाया जाना चाहिए कि प्रतिवादी का इरादा दूसरे पक्ष को झूठे बयान के माध्यम से अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना था। अंत में, यह साबित किया जाना चाहिए कि दूसरे पक्ष ने झूठे बयान पर भरोसा किया और परिणामस्वरूप उसे नुकसान उठाना पड़ा। यदि ये तत्व सिद्ध हो जाते हैं, तो पीड़ित पक्ष अनुबंध को रद्द कर सकता है और प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। कपटपूर्ण दुर्व्यपदेशन के मामले में क्षतिपूर्ति में आर्थिक नुकसान, जैसे कि जेब से किए गए खर्च और खोया हुआ लाभ, के लिए मुआवजा शामिल हो सकता है, साथ ही गैर-आर्थिक नुकसान, जैसे कि भावनात्मक संकट और प्रतिष्ठा को हुई क्षति के लिए मुआवजा भी शामिल हो सकता है।
लापरवाहीपूर्ण दुर्व्यपदेशन
किसी भी विक्रय अनुबंध में उचित सावधानी बरतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विक्रेता का दायित्व है कि वह क्रय हेतु प्रस्तुत माल के बारे में सटीक एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करे। इसके अलावा, किसी भी मौजूदा क्षति या दोष के बारे में ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। यदि विक्रेता किसी कथन की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उसे प्रस्तुत करता है, और वह कथन क्रेता के अनुबंध में प्रवेश करने के निर्णय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, तो क्रेता को झूठे विवरण के कारण हानि हो सकती है। ऐसे मामलों में, क्रेता को प्रदान की गई जानकारी का मूल्यांकन करते समय उचित सावधानी बरतने में विफल रहने की जिम्मेदारी लेनी होगी।
लापरवाहीपूर्ण दुर्व्यपदेशन के मामलों में क्रेता के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होते हैं। प्राथमिक तौर पर, क्रेता को अनुबंध को रद्द करने का अधिकार है, जिससे उसका अस्तित्व प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है। यह उपाय क्रेता को करार से हटने और माल विक्रेता को वापस करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, क्रेता विक्रेता के दुर्व्यपदेशन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के लिए मुआवजे की मांग कर सकता है। इन क्षतियों में वित्तीय नुकसान, भावनात्मक संकट, या झूठे बयान के कारण क्रेता को हुई कोई अन्य हानि शामिल हो सकती है।
लापरवाहीपूर्ण दुर्व्यपदेशन के मामले में सबूत का भार क्रेता पर होता है। क्रेता को यह प्रदर्शित करना होगा कि विक्रेता ने झूठा बयान दिया था, कि अनुबंध करते समय उन्होंने उस बयान पर भरोसा किया था, तथा विक्रेता के दुर्व्यपदेशन के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप उन्हें क्षति उठानी पड़ी थी। क्रेताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सामान खरीदते समय उचित सावधानी बरतें और सोच-समझकर निर्णय लें। गहन शोध, पेशेवर सलाह लेना, तथा अनुबंध की शर्तों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना, अपने हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। उचित सावधानी बरतकर, क्रेता लापरवाहीपूर्ण दुर्व्यपदेशन का शिकार होने के जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।
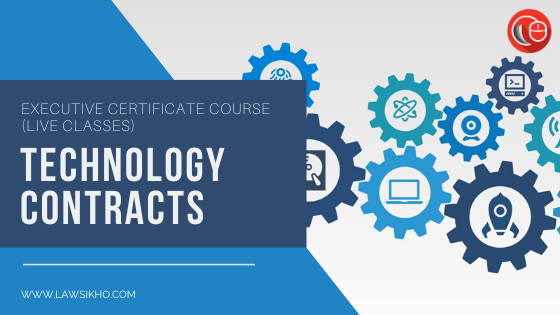
माल की बिक्री का अनुबंध
माल की बिक्री के लिए अनुबंध, माल बिक्री अधिनियम, 1930 द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम में विक्रय अनुबंध के निर्माण, ऐसे अनुबंध के प्रभाव, उसके निष्पादन, भुगतान करने वाले तथा न करने वाले विक्रेताओं के अधिकारों और कर्तव्यों तथा अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार संबंधी प्रावधान शामिल हैं।
माल की बिक्री के लिए एक अनुबंध में दो पक्ष शामिल होते हैं, एक क्रेता और दूसरा विक्रेता, जो एक अनुबंध बनाते हैं। इस अनुबंध में, विक्रेता एक निश्चित कीमत पर क्रेता को कुछ सामान हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। मूल्य हस्तांतरण के लिए प्रतिफल है। माल की बिक्री के अनुबंध के लिए दो पक्षों की उपस्थिति, एक हस्तांतरणीय माल और प्रतिफल के रूप में मूल्य आवश्यक हैं।
वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों में शामिल हैं:
- प्रस्ताव
- प्रस्ताव की स्वीकृति
- कानूनी संबंध बनाने का आशय
- प्रतिफल
माल की बिक्री के अनुबंध में दुर्व्यपदेशन
इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधान किसी भी माल की बिक्री के अनुबंध पर लागू होंगे, बशर्ते कि वह माल की बिक्री अधिनियम के किसी भी प्रावधान से असंगत न हो। यह प्रावधान माल की बिक्री के अनुबंध में गलत बयानी के मामले में भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति देता है। पीड़ित पक्ष न्यायालय में उपचार की मांग कर सकता है, हालांकि माल विक्रय अधिनियम में झूठे प्रतिनिधित्व के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
बिक्री का अनुबंध पूर्ण या सशर्त हो सकता है। अनुबंध को अंतिम रूप देने से पहले शर्तों पर चर्चा और बातचीत की जाती है। चर्चाओं और बातचीत के दौरान ही एक पक्ष दूसरे को प्रभावित करने में सक्षम होता है और इस स्तर पर दिया गया कोई भी बयान वैध और सुविचारित होना चाहिए, ताकि भविष्य में जोखिम से बचा जा सके।
अनुबंध बनाते समय विश्वसनीय बयान देना क्रेता तथा विक्रेता दोनों का कर्तव्य है। आंशिक सत्य या किसी भी चूक के बयान भी गलत प्रतिनिधित्व का कारण बनेंगे।
इस विषय पर आम सहमति
अनुबंध निर्माण के क्षेत्र में, किसी करार की वैधता के लिए एक मूलभूत आवश्यकता अनुबंध के विषय-वस्तु के संबंध में अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच साझा समझ या “सर्वसम्मति” है। यह साझा समझ यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष समान आशय और अपेक्षाओं के साथ अनुबंध में प्रवेश करें। हालाँकि, तथ्यों की ग़लतियाँ तब उत्पन्न हो सकती हैं जब विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच ग़लतफ़हमी या भ्रांति हो। ये गलतियां मूलतः दुर्व्यपदेशन हैं जो अनुबंध के लिए सहमति उत्पन्न करती हैं।
तथ्यों की ग़लतियाँ कई कारणों से हो सकती हैं। कभी-कभी, संचार संबंधी समस्याओं या समझ में अंतर के कारण विषय-वस्तु की ग़लतफ़हमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक पक्ष का मानना है कि वे कार का एक विशिष्ट मॉडल खरीद रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष एक अलग मॉडल बेचने का इरादा रखता है, तो तथ्य की गलती हुई है।
तथ्यों की गलतियों का एक अन्य सामान्य कारण महत्वपूर्ण तथ्यों का बहिष्करण या लोप है। यदि एक पक्ष महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने में विफल रहता है या विषय-वस्तु के बारे में गलत बयान देता है, तो यह दूसरे पक्ष को गलत धारणा के आधार पर अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि विक्रेता किसी उत्पाद में ज्ञात दोष का खुलासा करने में विफल रहता है, तो क्रेता यह गलत धारणा बनाकर उत्पाद खरीद सकता है कि इसमें कोई दोष नहीं है।
तथ्यों की गलतियों के महत्वपूर्ण कानूनी निहितार्थ हो सकते हैं। कुछ मामलों में, तथ्य की गलती अनुबंध को शून्य या शून्यकरणीय बना सकती है। यह बात विशेष रूप से तब सत्य है जब गलती अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण थी, अर्थात इसने करार के सार या तत्त्व को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, यदि तथ्य की कोई गलती विषय-वस्तु की पहचान से संबंधित है, जैसे कि मूल चित्रकारी के बजाय नकली चित्रकारी खरीदना, तो अनुबंध शून्य हो सकता है।
अन्य मामलों में, तथ्य की गलती के कारण अनुबंध शून्य नहीं हो सकता, लेकिन निरसन या क्षतिपूर्ति के लिए दावा उत्पन्न हो सकता है। निरसन, अनुबंध को रद्द करने या समाप्त करने की प्रक्रिया है, जिसमें पक्षों को अनुबंध में प्रवेश करने से पहले की उनकी मूल स्थिति में बहाल किया जाता है। दूसरी ओर, क्षतिपूर्ति का उद्देश्य उस पक्ष को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है जिसे गलती के कारण नुकसान हुआ है।
तथ्यों की गलतियों के जोखिम को कम करने के लिए, अनुबंध के पक्षों के लिए विषय-वस्तु के बारे में स्पष्ट और सटीक ढंग से संवाद करना महत्वपूर्ण है। उन्हें अनुबंध में प्रवेश करने से पहले प्रासंगिक तथ्यों की पूरी तरह से जांच और सत्यापन करके उचित परिश्रम भी करना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि दोनों पक्षों को विषय-वस्तु की सामान्य समझ हो तथा अनुबंध सटीक जानकारी पर आधारित हो।
शून्यकरणीय
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, जब कोई अनुबंध तथ्यों के झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा निर्मित किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष गलत प्रतिनिधित्व का पता चलने के बाद करार को रद्द करने का विकल्प चुन सकता है। मिथ्या-बयान द्वारा निर्मित अनुबंध शून्यकरणीय होता है; अन्यथा पीड़ित पक्ष अनुबंध के निष्पादन की मांग कर सकता है, मानो किया गया प्रतिनिधित्व सत्य था।
हालाँकि, किसी अनुबंध को शून्य घोषित करने के कुछ अपवाद हैं:
- यदि प्रतिवादी की चुप्पी के कारण महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के कारण सहमति प्राप्त की गई थी तो करार शून्यकरणीय नहीं होगा। यदि पीड़ित पक्ष के पास ऐसे झूठे प्रतिनिधित्व को पकड़ने की क्षमता और संसाधन थे, लेकिन उसने सच्चाई की जांच करने के लिए उचित सावधानी या तत्परता नहीं बरती, तो अनुबंध शून्यकरणीय नहीं होगा।
हॉर्सफॉल बनाम थॉमस (1862) के ऐतिहासिक मामले में, न्यायालय को इस जटिल मुद्दे पर विचार करना पड़ा कि क्या केवल दोष का खुलासा न करना मिथ्या प्रस्तुति या दुर्व्यपदेशन माना जाएगा।
मामला माल की बिक्री से जुड़ा था, जहां खरीदार, श्री हॉर्सफॉल ने विक्रेता, श्री थॉमस से तांबे की एक मात्रा खरीदी थी। श्री हॉर्सफॉल को पता नहीं था कि तांबे में एक गुप्त दोष था, जो इसे उसके इच्छित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त बनाता था। दोष का पता चलने के बाद, श्री हॉर्सफॉल ने श्री थॉमस के विरुद्ध दुर्व्यपदेशन और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था।

अदालत ने लेन-देन से जुड़ी परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच की तथा विक्रेता के आचरण पर विशेष ध्यान दिया। इसने निर्धारित किया कि श्री थॉमस ने जानबूझकर दोष को नहीं छिपाया था, बल्कि वह श्री हॉर्सफॉल को इसके बारे में बताने में असफल रहे थे। अदालत ने तर्क दिया कि किसी दोष का खुलासा न करना, अपने आप में, दुर्व्यपदेशन या धोखाधड़ी नहीं है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि उक्त दोष श्री थॉमस द्वारा छिपाया या छुपाया नहीं गया था। यह एक गुप्त दोष था, जो सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर पता चल गया। अदालत ने कहा कि श्री हॉर्सफॉल का यह दायित्व था कि वे अनुबंध में प्रवेश करने से पहले उचित सावधानी बरतें और माल की गहन जांच करें।
हॉर्सफॉल बनाम थॉमस मामले में न्यायालय के निर्णय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि विक्रेता केवल इस आधार पर गलत बयानी या धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी नहीं है कि उसने किसी दोष को प्रकट करने में विफलता दिखाई है, जिसे जानबूझकर नहीं छिपाया गया है। यह सिद्धांत वाणिज्यिक लेनदेन में कैविएट एम्प्टर, या “क्रेता सावधान रहें” के महत्व को रेखांकित करता है। इससे क्रेता पर यह दायित्व आ जाता है कि वह खरीदारी करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर ले और सामान का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कर ले।
फिर भी, अदालत के फैसले ने विक्रेताओं को अपने लेन-देन में ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया। यद्यपि दोष का खुलासा न करना गलत बयानी या धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता है, फिर भी विक्रेता सद्भावना और निष्पक्ष व्यवहार के कर्तव्य से बंधे होते हैं। वे खरीददारों को सक्रिय रूप से गुमराह नहीं कर सकते हैं या बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भ्रामक तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
हॉर्सफॉल बनाम थॉमस मामला दुर्व्यपदेशन और धोखाधड़ी के कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल बना हुआ है, जो इसी तरह के मामलों के विश्लेषण में अदालतों का मार्गदर्शन करता है। यह बेईमान विक्रेताओं से क्रेताओं की सुरक्षा और वाणिज्यिक लेनदेन में निष्पक्षता और निश्चितता को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- यदि दुर्व्यपदेशन के कारण सहमति नहीं दी गई है तो भी अनुबंध शून्यकरणीय नहीं है। जब क्रेता और विक्रेता के बीच किसी बिक्री पर चर्चा होती है, जिसमें विक्रेता मासूमियत से या धोखाधड़ी से कुछ गलत बयान करता है, तो क्रेता दुर्व्यपदेशन को पहचानने के बावजूद अनुबंध में प्रवेश करता है। इस मामले में, क्रेता ने जानबूझकर जोखिम उठाया, इसलिए बाद में अनुबंध को रद्द नहीं किया जा सकता है।
कानूनी उपाय
निरसन
निरसन एक उपाय है जो पक्षों को अनुबंध को समाप्त करने और अनुबंध बनने से पहले की अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस जाने की अनुमति देता है। यह अनुबंध को शून्य और निरर्थक बना देता है तथा गैर-उत्तरदायी पक्षों को उनके दायित्वों से मुक्त कर देता है। जब विक्रय अनुबंध रद्द कर दिया जाता है, तो खरीदी गई वस्तु विक्रेता को वापस कर दी जाएगी तथा विक्रेता को क्रेता को भुगतान की गई कीमत वापस करनी होगी।
प्रतिज्ञान
उपचार के रूप में प्रतिज्ञान को लागू करने के लिए, पीड़ित पक्ष को दुर्व्यपदेशन या अनुबंध के उल्लंघन के बारे में पता होना चाहिए। जब तक समय है, यदि वे पुष्टि करना चाहते हैं, तो अनुबंध जारी रहेगा, जैसे कि दुर्व्यपदेशन सच थी। हालाँकि, यदि दावेदार अनुबंध के उल्लंघन के बाद लंबे समय तक इसे रद्द करने या पुष्टि करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो यह माना जाता है कि वह पुष्टि करता है और अनुबंध जारी रखना चाहता है।
दुर्व्यपदेशन के इस मामले में, वादी ने कुछ खामियों को देखते हुए प्रतिवादी से आधी कीमत पर एक लॉरी खरीदी थी। वादी को ट्रक के माइलेज में कुछ गंभीर समस्याएं नजर आईं और उसने इसकी सूचना प्रतिवादी को दी, जिसके बाद ट्रक खराब हो जाने पर उसने उसे अपने भाई को व्यापारिक यात्रा के लिए दे दिया। इस घटना के बाद, वादी अनुबंध को रद्द करना चाहता था। हालांकि, अदालत ने वादी के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि जब निर्दोष दुर्व्यपदेशन का पता चला तो वादी के पास इसे रद्द करने का अवसर था; हालांकि, उसने इसका उपयोग करना जारी रखा और यहां तक कि इसे अपने भाई को उधार भी दे दिया; भाई को इसे उधार देना पुष्टि का कार्य माना गया था।
माल की बिक्री के अनुबंध में, दुर्व्यपदेशन के दावे से निपटने के लिए दायित्व की सीमाएं और उपचार शामिल किए जा सकते हैं। अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार और दायित्व को सीमित करने वाला खंड उचित और निष्पक्ष होना चाहिए।
धोखाधड़ी और दुर्व्यपदेशन के बीच अंतर
धोखाधड़ी और दुर्व्यपदेशन दोनों ही जानबूझकर किए गए कार्य हैं जो दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच प्रमुख अंतर हैं।
धोखाधड़ी – धोखाधड़ी एक जानबूझकर किया गया कार्य है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को धोखा देना होता है। इसमें झूठ बोलना, धोखा देना या चोरी करना शामिल हो सकता है। धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य आपराधिक या दीवानी हो सकते हैं, और इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे जुर्माना, कारावास या प्रतिष्ठा की हानि।
दुर्व्यपदेशन – दुर्व्यपदेशन एक व्यापक शब्द है जो किसी भी मिथ्या कथन या तथ्य की चूक को शामिल करता है। यह जानबूझकर या अनजाने में हो सकता है, और यह भौतिक या अभौतिक भी हो सकता है। भौतिक दुर्व्यपदेशन वे हैं जिनसे किसी व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है, जबकि अभौतिक दुर्व्यपदेशन वे हैं जिनसे कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होती है।
मुख्य अंतर – धोखाधड़ी और दुर्व्यपदेशन के बीच मुख्य अंतर ये हैं:
- आशय: धोखाधड़ी हमेशा जानबूझकर की जाती है, जबकि दुर्व्यपदेशन जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है।
- भौतिकता: धोखाधड़ी वाले कार्य हमेशा भौतिक होते हैं, जबकि दुर्व्यपदेशन भौतिक या अभौतिक हो सकते हैं।
- परिणाम: धोखाधड़ी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे जुर्माना, कारावास या प्रतिष्ठा की हानि, जबकि दुर्व्यपदेशन के कोई भी परिणाम नहीं हो सकते हैं।
उदाहरण – धोखाधड़ी और दुर्व्यपदेशन के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:
- धोखाधड़ी: यदि कोई कार विक्रेता पुरानी कार की स्थिति के बारे में झूठ बोलता है तो वह धोखाधड़ी कर रहा है।
- दुर्व्यपदेशन: जो नौकरी का आवेदक अपने जीवनवृत्तांत (बायोडाटा) में अपनी योग्यताओं को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है, वह दुर्व्यपदेशन कर रहा है।
- धोखाधड़ी: जो कंपनी जानबूझकर दोषपूर्ण उत्पाद बेचती है, वह धोखाधड़ी कर रही है।
- दुर्व्यपदेशन: यदि कोई रेस्टॉरेंट किसी व्यंजन को “ताज़ी सामग्री से बना” बताकर विज्ञापित करता है, जबकि वह वास्तव में जमे हुए सामग्रियों से बना होता है, तो वह दुर्व्यपदेशन कर रहा है।

निष्कर्ष
दुर्व्यपदेशन एक ऐसा झूठा कथन है जो किसी अनुबंध को बनाते समय दिया जाता है या दर्शाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ देने से गलत बयानी संभव है। इससे अनुबंध के एक पक्ष को हानि हो सकती है, जबकि दूसरे पक्ष को कुछ लाभ हो सकता है। अनुबंध बनाते समय सभी तथ्यों और कथनों की जांच करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तथ्य विश्वसनीय और सत्य हैं। मिथ्या कथन मासूमियत से या लापरवाही से या धोखाधड़ी के आशय से दिए जा सकते हैं, एक सक्षम पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह करार करने से पहले सभी उचित सावधानियां बरतें। दैनिक जीवन में हर व्यक्ति द्वारा सामान बेचा और खरीदा जाता है; सामान खरीदते समय सोच-समझकर निर्णय लिया जाना चाहिए। मिथ्या प्रतिनिधित्व किसी पक्ष को ऐसा अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे वह अन्यथा नहीं करता; तथापि, मिथ्या प्रतिनिधित्व का पता चलने पर, पीड़ित पक्ष के पास अनुबंध को रद्द करने या उसे पुष्ट करने तथा अनुबंध को जारी रखने की मांग करने का विकल्प होता है। दुर्व्यपदेशन अनुबंध के उल्लंघन का आधार है।
संदर्भ







