यह लेख Matisa Majumder द्वारा लिखा गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रेक्ट, नेगोसिएशन, ड्राफ्टिंग एंड एनफोर्समेंट में डिप्लोमा कर रहे हैं। इस लेख मे अनुबंध और सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन) और भारत में न्यायिक निहितार्थ के बारे मे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
अनुबंध किसी भी आर्थिक प्रणाली में वाणिज्यिक लेनदेन और कानूनी करारों की नींव का काम करते हैं। उनका महत्व यह सुनिश्चित करने में निहित है कि कानूनी लेनदेन में शामिल सभी पक्षों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, जिससे विवादों को सुलझाने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध हो सके। भारत में, कानूनी प्रणाली ने अनुबंध संबंधी विवादों की एक विस्तृत श्रृंखला को सुलझाने के लिए लगातार विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया है। इन सिद्धांतों में, सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत विशेष महत्व रखता है।
सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी अनुबंधात्मक विवाद में शामिल पक्षों के बीच एक नया करार हो जाता है, तो मूल अनुबंध प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है या संशोधित हो जाता है। यह नया करार, जिसे सहमति के रूप में जाना जाता है, में आम तौर पर मूल अनुबंधात्मक दायित्वों को नए नियमों या शर्तों के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। दूसरी ओर, संतुष्टि का तात्पर्य इन नई शर्तों या नियमों की पूर्ति से है।
सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की पूर्ति की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, मूल अनुबंध की शर्तों या निष्पादन के संबंध में पक्षों के बीच वास्तविक विवाद या असहमति होनी चाहिए। दूसरा, पक्षों के बीच एक नया करार या सहमति होना चाहिए, जो मूल अनुबंधात्मक दायित्वों को परिवर्तित या संशोधित कर दे। तीसरा, संतुष्टि तत्व तब सामने आता है जब करार में सहमत नई शर्तों या नियमों का पालन किया जाता है या उन्हें पूरा किया जाता है। यह आवश्यक है कि संतुष्टि दोनों पक्षों की सहमति से निष्पादित की जाए।

भारत में अनुबंधों को समझना
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, भारत में अनुबंधात्मक लेन-देन की आधारशिला के रूप में कार्य करता है तथा उन्हें व्यापक रूप से परिभाषित और विनियमित करता है। मूलतः, एक अनुबंध में एक पक्ष द्वारा किया गया प्रस्ताव, दूसरे पक्ष द्वारा उस प्रस्ताव की स्वीकृति, दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किया गया मूल्यवान प्रतिफल, तथा करार में कानूनी रूप से आबद्ध होने का पारस्परिक आशय शामिल होता है।
अधिनियम अनुबंधों को उनकी विशेषताओं और कानूनी निहितार्थों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अभिव्यक्त अनुबंध वे होते हैं जो लिखित या मौखिक रूप में स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं। दूसरी ओर, निहित अनुबंधों का अनुमान इसमें शामिल पक्षों के आचरण और कार्यों से लगाया जाता है, भले ही स्पष्ट मौखिक या लिखित संचार न हो।
आकस्मिक अनुबंध वे होते हैं जिनमें अनुबंध की प्रवर्तनीयता या पूर्ति किसी विशिष्ट भविष्य की घटना के घटित होने या न घटित होने पर निर्भर करती है। शून्य अनुबंध वे होते हैं जो अवैधता, पक्षों की अक्षमता या धोखाधड़ी जैसे कारकों के कारण शुरू से ही कानूनी रूप से अमान्य होते हैं। शून्यकरणीय (वॉयडेबल) अनुबंध, प्रारंभ में वैध होते हुए भी, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव या गलती जैसे कारकों के कारण एक या दोनों पक्षों के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाते हैं।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 भारतीय क्षेत्र में अनुबंधों के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तन के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करता है। यह किसी अनुबंध को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए आवश्यक तत्वों और शर्तों को रेखांकित करता है तथा अनुबंध की शर्तों की व्याख्या और अर्थ लगाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है।
अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में, अधिनियम पीड़ित पक्ष को उपचार प्रदान करता है। इन उपायों में क्षतिपूर्ति शामिल है, जो उल्लंघन न करने वाले पक्ष को उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुई हानि की भरपाई करती है। विशिष्ट निष्पादन, जो उल्लंघन करने वाले पक्ष को सहमति के अनुसार अपने अनुबंधों के दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है, कुछ परिस्थितियों में भी मांगा जा सकता है। निषेधाज्ञा (इंजंक्शन), जो न्यायालय के आदेश होते हैं, किसी पक्ष को किसी विशिष्ट कार्य को करने या जारी रखने से रोकते हैं, उल्लंघन के कारण होने वाली आगे की हानि या अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए दी जा सकती है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 अनुबंधात्मक संबंधों में निष्पक्षता, निश्चितता और पूर्वानुमेयता (प्रिडिक्टेबिलिटी) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यवसायों, व्यक्तियों और कानूनी पेशेवरों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि अनुबंध इस प्रकार से किए जाएं और उनका निष्पादन इस प्रकार से किया जाए कि इसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों और हितों की रक्षा हो।
हमारे भारतीय कानून में सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। लेकिन उक्त सिद्धांत भारतीय न्याय व्यवस्था से छिपा नहीं है। हमारी न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में विभिन्न अनुबंधात्मक विवादों में स्पष्टीकरण और राहत प्रदान करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया है, जिससे हमें कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है।
सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत को परिभाषित करना
ऐसे कई तरीके हैं जिनसे कोई पक्ष अपने अनुबंधात्मक दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। ऐसी ही एक विधि है सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत, जिसके द्वारा पक्षों को कुछ संशोधित दायित्वों या शर्तों का पालन करके अपने अनुबंधात्मक दायित्वों का निर्वहन करने की अनुमति दी जाती है। पुराने करार के स्थान पर नया करार करने से पुराने करार के तहत शेष बचे दायित्वों का निर्वहन हो जाता है। करार अनुबंध की नई शर्तों पर सहमति है और संतुष्टि अनुबंध के अनुसार उन शर्तों का निष्पादन है। जब सहमति हो जाती हैं और संतुष्टि प्रदान कर दी जाती है, तो मूल अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन हो जाता है और मूल अनुबंध के तहत कोई नया दावा नहीं किया जा सकता है।
यह सिद्धांत तब लाभदायक होता है जब पक्ष मुकदमों से जुड़े समय, लागत, विलंब और अनिश्चितता से बचना चाहते हैं। यह पक्षों की आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है, जो लम्बी अदालती लड़ाइयों की तुलना में त्वरित और लागत प्रभावी है।
सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत के घटक
आइये सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत के प्रमुख घटकों का विश्लेषण करें:
सहमति या करार
इस सिद्धांत का पहला घटक यह है कि विवाद को निपटाने के लिए पक्षों के बीच एक करार होता है। यह करार स्पष्ट, अस्पष्ट तथा दोनों पक्षों द्वारा नई शर्तों की समझ के साथ पारस्परिक सहमति से होना चाहिए। यहां यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से तथा विवादों को सुलझाने के आशय से नई शर्तों पर पारस्परिक सहमति दें।
प्रतिफल
किसी भी अनुबंध की तरह, इसके वैध होने के लिए प्रतिफल की आवश्यकता होती है। सहमति के वैध होने के लिए भी प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल से हमारा तात्पर्य है कि पक्षों के बीच आपसी सहमति से किसी मूल्यवान वस्तु का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। यह धन, वस्तु, सेवा या मूल्य के किसी अन्य रूप में हो सकता है।
संतुष्टि निष्पादन
करार का निष्पादन इस सिद्धांत का एक अन्य प्रमुख घटक है। जब सहमत शर्तों के अनुसार कार्य पूरे हो जाते हैं, तो संतुष्टि होती है। करार का निष्पादन या तो भुगतान पूरा करके या माल या सेवाओं का वितरण करके या किसी अन्य सहमत वितरण के द्वारा किया जा सकता है। एक बार संतुष्टि हो जाने पर मूल करार रद्द कर दिया जाता है।
मूल दायित्वों का निर्वहन
इस सिद्धांत का अंतिम घटक मूल अनुबंध के तहत दायित्वों का निर्वहन है। जैसा कि पिछले घटक में बताया गया है, एक बार जब नई सहमत शर्तों का निष्पादन पूरा हो जाता है, तो मूल अनुबंधात्मक दायित्व समाप्त हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो मूल अनुबंध अब पक्षों के बीच बाध्यकारी नहीं है। इसलिए, कोई भी व्यक्ति पिछले अनुबंध के आधार पर कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह लागू नहीं होता है।
सहमति और संतुष्टि हो जाने पर, विवाद का समाधान मान लिया जाता है।
छूट के सिद्धांत और सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत में अंतर
सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत और छूट के सिद्धांत दोनों का उपयोग अनुबंधात्मक विवादों के निपटान के लिए किया जाता है। लेकिन इन दोनों सिद्धांतों के अनुप्रयोग और निहितार्थ भिन्न हैं।

- सबसे पहले, करार की प्रकृति। सहमति के सिद्धांत के मामले में, विवाद को निपटाने के लिए एक नया करार किया जाता है और उस करार के निष्पादन के परिणामस्वरूप मूल करार के दायित्वों का निर्वहन हो जाता है। लेकिन छूट के मामलों में, मूल करार के तहत किसी अधिकार या दावे का स्वैच्छिक त्याग होता है। छूट किसी अधिकार को छोड़ने का एक जानबूझकर किया गया कार्य है; इसमें कोई नया करार शामिल नहीं होता है।
- दूसरा, दोनों करार में प्रतिफल शामिल है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत के लिए, प्रतिफल एक महत्वपूर्ण घटक है और नई शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने की आवश्यकता है। लेकिन छूट के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं हो सकता है। छूट एकपक्षीय भी हो सकती है, जिसमें एक पक्ष बिना किसी नए प्रतिफल के अपने अधिकार को त्याग देता है।
- तीसरा, मूल करार के तहत दावे शामिल है। सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत के अनुसार, यह स्पष्ट है कि जब नई शर्तों पर आधारित करार का निष्पादन पूरा हो जाता है, तो मूल अनुबंध समाप्त हो जाता है। जबकि छूट के सिद्धांत के मामले में, यह आवश्यक रूप से मूल अनुबंध को समाप्त नहीं करता है। यह करार के तहत केवल कुछ अधिकारों को समाप्त करता है तथा करार का शेष भाग वैध और लागू करने योग्य रहता है।
भारत और यूके और अमेरिका की रूपरेखा मे अंतर
भारत में, सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत की कानूनी ढांचे में सीधी उपस्थिति नहीं है, लेकिन कानूनी प्रणाली द्वारा इसे मान्यता दी गई है। भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में इस सिद्धांत को बरकरार रखा है, तथा पुराने करारों के निर्वहन के लिए आपसी सहमति और नई शर्तों की पूर्ति के महत्व पर बल दिया है। आइए अब दो प्रमुख आर्थिक राष्ट्रों के कानूनी ढांचे पर नजर डालें और सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत की उनकी समझ पर नजर डालें।
यूनाइटेड किंगडम (यू.के.)
यूनाइटेड किंगडम में, सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत सामान्य कानून ढांचे के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कानूनी सिद्धांत यह मानता है कि किसी मौजूदा अनुबंधात्मक दायित्व का निर्वहन, संबंधित पक्षों के बीच एक नए करार की स्थापना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हालाँकि, इस नए करार को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने और पुराने अनुबंध को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
एक मूलभूत आवश्यकता यह है कि नए करार पर दोनों पक्षों को स्वेच्छा से पहुंचना होगा। स्वैच्छिकता का यह तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से तथा किसी भी प्रकार के दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना नए करार में प्रवेश करें। अदालतें पक्षों के बीच वास्तविक और पारस्परिक सहमति स्थापित करने पर बहुत जोर देती हैं।
इसके अलावा, नए करार की शर्तों पर पारस्परिक सहमति होनी चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों को नई व्यवस्था से उत्पन्न होने वाले अधिकारों और दायित्वों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। यह स्पष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि करार की शर्तों के संबंध में कोई अस्पष्टता या गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि नया करार पुराने अनुबंध का स्थान लेता है। एक बार नया करार स्थापित हो जाने पर, मूल अनुबंधात्मक दायित्व समाप्त हो जाते हैं, तथा पक्ष अब नए समझौते की शर्तों से बंध जाते हैं। यह सिद्धांत विवादों और अनुबंधात्मक मुद्दों के व्यवस्थित और सहमतिपूर्ण समाधान की अनुमति देता है, तथा कानूनी संबंधों में निष्पक्षता और निश्चितता को बढ़ावा देता है।
अंग्रेजी अदालतों ने लगातार स्वैच्छिक आशय और सहमति और संतुष्टि करारों में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों को स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया है। यह जोर इस बात को सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करता है कि दोनों पक्ष वास्तव में पुराने अनुबंध को समाप्त करने का इरादा रखते हैं और उन्हें नए करार की शर्तों की स्पष्ट समझ है।
संक्षेप में, सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत, जैसा कि यूके के सामान्य कानून में मान्यता प्राप्त है, नए करारों के निर्माण के माध्यम से अनुबंधात्मक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस सिद्धांत का आधार स्वैच्छिकता और पारस्परिक सहमति के सिद्धांतों पर आधारित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इसमें शामिल पक्ष स्वतंत्र रूप से और इसकी शर्तों की स्पष्ट समझ के साथ नए करार में प्रवेश करें। न्यायालयों द्वारा इन तत्वों पर जोर देने से सहमति और संतुष्टि करारों की अखंडता और प्रवर्तनीयता को बनाए रखने में मदद मिलती है, तथा अनुबंधात्मक संबंधों में निष्पक्षता और निश्चितता को बढ़ावा मिलता है। इस सिद्धांत से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला ब्रिटिश रूसी गैजेट लिमिटेड बनाम एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स लिमिटेड (1933) था, जहां अदालत ने माना कि सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत तभी वैध है जब विवाद को निपटाने के लिए पक्षों के बीच वास्तविक करार हो, जो प्रतिफल द्वारा समर्थित हो, और यदि संतुष्टि विधिवत निष्पादित की गई हो। यह मामला इस बात पर जोर देता है कि मूल अनुबंध को समाप्त करने के लिए, नया अनुबंध स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए तथा सहमत शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए।
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए)
संयुक्त राज्य अमेरिका में, सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत का उपयोग अनुबंध के प्रकार के आधार पर किया गया है। उक्त सिद्धांत वाणिज्यिक अनुबंधों के लिए समान वाणिज्यिक संहिता (यूसीसी) और अन्य अनुबंधों के लिए सामान्य कानून द्वारा शासित होता है। यूसीसी सहमति और संतुष्टि के लिए स्पष्ट प्रावधान प्रदान करता है, मुख्य रूप से परक्राम्य लिखतों (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) जैसे चेक, वचन पत्र, विनिमय पत्र आदि के संदर्भ में है। यह सिद्धांत लागत दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए विवादों के निपटारे के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
इस सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला हॉर्न वॉटरप्रूफिंग कार्पोरेशन बनाम बुशविक आयरन एंड स्टील कंपनी इनकॉरपोरेशन (1985) है, जिसमें न्यूयॉर्क अपील न्यायालय ने कहा कि सहमति और संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब पक्ष नए अनुबंध के लिए पारस्परिक रूप से सहमत होते हैं और दायित्वकर्ता नए करार की शर्तों का पालन करता है, जिससे मूल अनुबंध समाप्त हो जाता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नए करार (सहमति) और उसके निष्पादन (संतुष्टि) दोनों के लिए स्पष्ट साक्ष्य मूल अनुबंध को समाप्त करने के लिए आवश्यक है।
भारत में न्यायिक निहितार्थ
हमारी न्यायपालिका अक्सर उन सिद्धांतों को कायम रखने में अग्रणी रही है, जो संहिताबद्ध (कॉड़ीफाइड) कानूनी ढांचे में अक्सर छूट जाते हैं। यह सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत से भी स्पष्ट है, जिस पर भारतीय न्यायपालिका ने लगातार चर्चा की है और समय-समय पर इसकी वैधता को बरकरार रखा है।
हमारी भारतीय न्यायपालिका के कुछ ऐतिहासिक निर्णय नीचे दिए गए हैं:
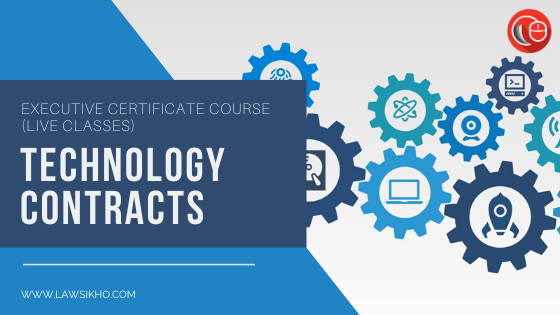
- हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1999) के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत की वैधता को बनाए रखने में आपसी सहमति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया था। यह सिद्धांत, अनुबंध कानून के सिद्धांतों पर आधारित है, तथा यह पक्षों के एक नए करार के माध्यम से मौजूदा अनुबंधात्मक दायित्वों को संशोधित करने या समाप्त करने की क्षमता को मान्यता देता है।
अदालत के निर्णय का मुख्य बिन्दु यह था कि नई शर्तों पर दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति आवश्यक है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सहमति या नया करार स्वतंत्र रूप से और सहमति से किया जाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि पक्ष समान स्तर पर हों तथा उनकी सहमति वास्तविक और सूचित हो।
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि मात्र बातचीत या चर्चा, भले ही उनमें नई शर्तों का प्रस्ताव शामिल हो, स्वतः ही सहमति नहीं बन जाती है। किसी सहमति को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के लिए, दोनों पक्षों द्वारा नई शर्तों को स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। यह स्वीकृति स्पष्ट बयानों, लिखित करार या आचरण के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है जो नए करार से बंधे रहने की मंशा को प्रदर्शित करती है।
आपसी सहमति की आवश्यकता के अतिरिक्त, न्यायालय ने संतुष्टि, या नए करार के निष्पादन के महत्व पर भी बल दिया। अदालत के अनुसार, संतुष्टि का कार्य नए करार की शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मूल अनुबंधात्मक दायित्वों को समाप्त करने के लिए पक्षों को नए करार के तहत अपने-अपने दायित्वों को पूरा करना होगा।
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य मामले में न्यायालय का निर्णय सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए एक मूल्यवान मिसाल के रूप में कार्य करता है। पारस्परिक सहमति के सिद्धांतों और संतुष्टि की आवश्यकता पर जोर देकर, न्यायालय अनुबंध संबंधी विवादों को सुलझाने और नए करारों के माध्यम से मौजूदा दायित्वों के संशोधन या समाप्ति को सुगम बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह निर्णय अनुबंधात्मक संबंधों में निष्पक्षता, निश्चितता और प्रवर्तनीयता बनाए रखने में योगदान देता है।
- भारत संघ बनाम किशोरीलाल गुप्ता एवं ब्रदर्स (1960): इस मामले ने सहमति में प्रतिफल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बिना प्रतिफल के दी गई सहमति प्रवर्तनीय नहीं है, तथा मूल अनुबंध तब तक प्रभावी रहता है जब तक वैध प्रतिफल प्रदान नहीं किया जाता है तथा संतुष्टि प्रदान नहीं की जाती है।
- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009): इस मामले में इस बात पर जोर दिया गया कि वैध सहमति और संतुष्टि के लिए विवाद को निपटाने के लिए स्पष्ट और स्वैच्छिक करार होना चाहिए तथा नई शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे यह पुष्ट होता है कि इस सिद्धांत की वैधता के लिए आपसी सहमति महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि स्वीकृति स्वतंत्र सहमति के बिना की गई है तो मात्र कम राशि की स्वीकृति सहमति और संतुष्टि नहीं है।
चुनौतियां
किसी भी अन्य सिद्धांत की तरह सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत भी अपनी चुनौतियों के साथ आता है, जहां इस सिद्धांत की प्रयोज्यता कम पड़ जाती है। इनमें से कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं:
- अस्पष्ट करार: चूंकि सहमति नए अनुबंध पर करार है, इसलिए यहां प्रमुख चुनौती स्पष्ट शर्तें हैं। नई शर्तों पर स्पष्टता का अभाव विवादों को जन्म दे सकता है, जिससे सहमति की प्रभावशीलता कम हो सकती है।
- प्रवर्तन: नये करार का प्रवर्तन अपने आप में एक चुनौती है। यदि कोई पक्ष नई शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो करार को लागू करने योग्य नहीं माना जा सकता है।
- आपसी सहमति: दोनों पक्षों को स्वेच्छा से नई शर्तों को स्वीकार करना चाहिए; अन्यथा, नई शर्तों की वैधता समाप्त हो जाएगी। पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए।

निष्कर्ष
भारतीय अनुबंध कानून में सहमति और संतुष्टि का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यह पक्षों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जिससे लंबे विवादों से बचा जा सकता है। यह निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, मुकदमेबाजी को कम करता है, लागत प्रभावी है, तथा अनुबंधात्मक दावों में शामिल पक्षों को निश्चितता प्रदान करता है। यद्यपि नए अनुबंध पर स्पष्ट प्रारूपण (ड्राफ्टिंग), प्रभावी प्रवर्तन, तथा आपसी सहमति पर स्वैच्छिक सहमति जैसी चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी इन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। सहमति और संतुष्टि के सिद्धांत को समझकर, पक्ष अपने विवादों को कुशलतापूर्वक और न्यायसंगत तरीके से सुलझा सकते हैं, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण कानूनी वातावरण का निर्माण हो सकता है।
संदर्भ







