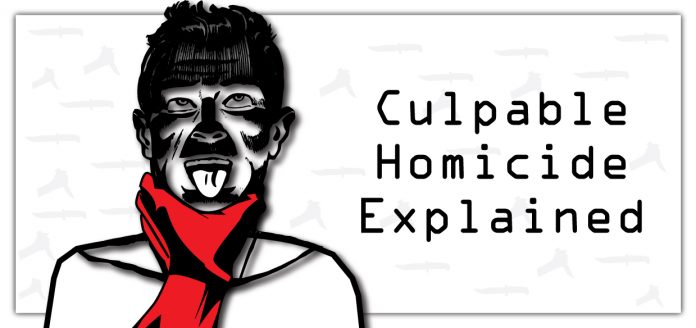यह लेख Yashovardhan Agarwal द्वारा लिखा गया है, और आगे Jaanvi Jolly द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया। यह लेख भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रदान की गई आपराधिक मानव वध (कल्पेबल होमिसाइड) की अवधारणा से विस्तृत रूप से निपटने का प्रयास करता है और संबंधित मामलों की मदद से इससे संबंधित कई बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करता है। इसके अलावा, ‘कल्पित परिस्थितियों (सपोज़्ड सरकमस्टैन्स)’ की अवधारणा और ‘द्वेष के हस्तांतरण (ट्रान्स्फर ऑफ मैलिस)’ के सिद्धांत को भी समझाया गया है। यह बचाव के रूप में उकसावे के क्षेत्र में ‘पीड़ित महिला सिंड्रोम’ की अवधारणा को पेश करने का भी प्रयास करता है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
“मानव वध” को अंग्रेजी में होमीसाइड कहा जाता है यह शब्द लैटिन शब्द “होमो” जिसका अर्थ है मानव, और “सेडरे” जिसका अर्थ है मारना, से आया है,। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या करना एक ऐसी घटना है जिसकी जड़ें मानव जाति की शुरुआत से ही है, प्रकृति की अवस्था में वापस जाती हैं।
मानव वध हमेशा दंडनीय नहीं होता; मृत्युदंड के किसी आदेश के क्रियान्वयन या निजी बचाव के किसी कार्य के बारे में सोचें जो दुर्भाग्य से दूसरे की मृत्यु का कारण बनता है। इन उदाहरणों में, चूंकि हमारे पास उचित आधार हैं तो किसी आपराधिक मनःस्थिति (मेंस रिया) को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए इन्हें वैध मानव वध कहा जाता है। हालाँकि, उचित आधार के अभाव में, दूसरे की हत्या गैरकानूनी और दंडनीय है। ‘गैरकानूनी मानव वध’ या ‘आपराधिक मानव वध’ का क्षेत्र इस लेख का विषय है।
1860 का पूर्व भारतीय दंड संहिता (आईपीसी,1860) के अध्याय XVI और नव प्रस्तुत भारतीय न्याय संहिता, 2023 (इसके बाद बीएनएस, 2023) के अध्याय VI के तहत शरीर के खिलाफ अपराधों से व्यापक रूप से निपटते हैं, जिनमें से आपराधिक मानव वध एक हिस्सा है। भारत में, आपराधिक मानव वध को दो रूपों में विभाजित किया गया है: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 100 के तहत ‘आपराधिक मानव वध’ (पूर्व में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 299) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 101 के तहत ‘आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी मे आते है’ (पूर्व में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300)।
प्रथम दृष्टया पढ़ने पर, दोनों बहुत समान लग सकते हैं; हालांकि, इरादे की डिग्री में बहुत महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिन्हें अवधारणाओं की बेहतर समझ के लिए समझना होगा। इन अंतरों को लेख में उपयुक्त स्थानों पर विस्तृत रूप से बताया गया है। इन अवधारणाओं को समझने के बाद, कोई भी यह विश्लेषण करने और समझने में सक्षम होगा कि कौन सा कार्य हत्या के अपराध के अंतर्गत आएगा और कौन सा कार्य आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी में नहीं आते है, उन तक सीमित होगा।

नए शुरू किए गए बीएनएस, 2023 द्वारा केवल प्रावधानों की धारा संख्या बदल दी गई है और धारा के शब्दों में कोई बदलाव नहीं है। तुलना के लिए नए और पुराने धारा संख्या नीचे तालिका में दिए गए हैं।
| अपराध | भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धाराएँ | भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धाराएँ |
| आपराधिक मानव वध | धारा 100 | धारा 299 |
| हत्या | धारा 101 | धारा 300 |
| जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनकर आपराधिक मानव वध – द्वेष का स्थानांतरण | धारा 102 | धारा 301 |
| हत्या के लिए सज़ा | धारा 103 | धारा 302 |
| आजीवन कारावास की सजा पाए गए व्यक्ति के द्वारा हत्या करने पर सजा | धारा 104 | धारा 303 |
| आपराधिक मानव वध के लिए सजा | धारा 105 | धारा 304 |
आपराधिक मानव वध
बीएनएस, 2023 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए, तीन तत्व मौजूद होने चाहिए:
- आपराधिक मनःस्थिति: जो अपराध के लिए आवश्यक दोषी दिमाग या दोषी इरादा है। आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए या तो इरादा या पूर्व जानकारी मौजूद होना चाहिए। यह,”एक्टस रीअस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, के आपराधिक कानून सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है “एक कार्य एक व्यक्ति को अपराध का दोषी नहीं बनाता है जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो।”
दिप्ता दत्ता बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2023), के मामले में यह कहा गया था कि, ‘आपराधिक मनःस्थिति‘ मन की स्थिति है जो दोषीता को इंगित करती है, जो अपराध के एक तत्व के रूप में एक क़ानून द्वारा आवश्यक है। प्रत्येक अपराध के लिए एक मानसिक तत्व की आवश्यकता होती है जो कि कोई निंदनीय मानसिक स्थिति होती है।
हालाँकि ‘आपराधिक मनःस्थिति‘ शब्द आईपीसी 1860 या बीएनएस 2023 में कहीं नहीं पाया गया है, इसका सार संहिता के लगभग सभी प्रावधानों में अभिव्यक्तियों के उपयोग से परिलक्षित होता है जैसे: “इरादे से, जानबूझकर, लापरवाही से, गैरकानूनी, दुर्भावनापूर्ण, जानकर या विश्वास करके, धोखाधड़ी से, बेईमानी से, आदि।”
- आपराधिक कार्य: जो अपराध के लिए आवश्यक दोषी कार्य या चूक है। आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए।
- आकस्मिकता का तत्व: अभियुक्त का कार्य अपेक्षित आपराधिक मनःस्थिति के तहत किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपराधिक मानव वध के अपराध के लिए ‘मृत्यु कारित करने का कार्य’ ‘मृत्यु कारित करने के इरादे या ज्ञान’ के साथ किया जाना चाहिए।
आपराधिक मानव वध की डिग्री
आचरण की गंभीरता और इसमें शामिल अपराध के कारण के आधार पर आपराधिक मानव वध को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:
- पहली डिग्री– यह आपराधिक मानव वध का सबसे गंभीर रूप है, जिसे बीएनएस, 2023 की धारा 101 में हत्या के रूप में परिभाषित किया गया है और बीएनएस, 2023 की धारा 103 में इसे दंडनीय बनाया गया है।
- दूसरी डिग्री– यह बीएनएस, 2023 की धारा 100 में परिभाषित आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी में नहीं आते है, उनका कम गंभीर रूप है और इसे बीएनएस, 2023 की धारा 105 के पहले भाग के तहत दंडनीय बनाया गया है।
- तीसरी डिग्री– यह आपराधिक मानव वध का सबसे कम गंभीर रूप है। इसे भी बीएनएस, 2023 की धारा 100 के तहत परिभाषित किया गया है और बीएनएस, 2023 की धारा 105 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय है।
संहिता की योजना में, आपराधिक मानव वध ‘जाति‘ है जबकि हत्या ‘प्रजातियाँ‘, है। सभी हत्याएं आपराधिक मानव वधएं हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानव वध हत्या नहीं हैं। इसलिए, हत्या की विशेष विशेषताओं के बिना आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध है, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है ।
अगले खंड में हम आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी में नहीं आते है, उनके अपराध और अपराध के लिए सज़ा का विश्लेषण करके शुरुआत करेंगे।
आपराधिक मानव वध, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता: बीएनएस, 2023 की धारा 100 (आईपीसी, 1860 की धारा 299)
कोई भी कार्य दो परिस्थितियों में आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी में नहीं आते है, इसके अंतर्गत आ सकता है:
- आपराधिक मानव वध, जो कभी भी हत्या बनने की सीमा पार नहीं कर पाया, या
- आपराधिक मानव वध, जो हत्या की सीमा को पार कर गया, लेकिन बीएनएस, 2023 की धारा 101 के तहत प्रदान किए गए कोई भी अपवाद लागू थे, जिससे आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, उसमे बदल दिया गया।
ये दोनों स्थितियाँ बीएनएस, 2023 की धारा 105 के तहत दंडनीय हैं।
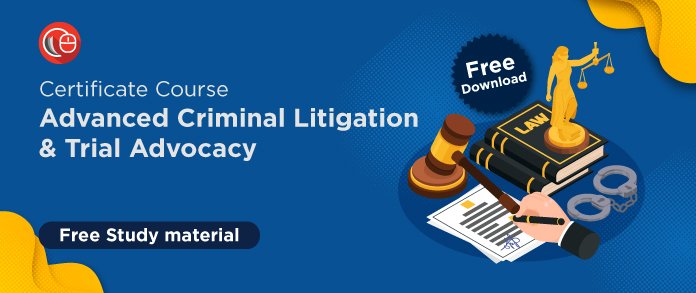
बीएनएस, 2023 की धारा 100 में तीन वाक्यांश शामिल हैं जो अलग-अलग मानसिकता और अलग-अलग आचरण को दर्शाते हैं। ये इस प्रकार हैं:
- मृत्यु कारित करने का इरादा
- ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मृत्यु होने की संभावना हो
- उस कार्य का ज्ञान जिससे मृत्यु होने की संभावना हो
तीन वाक्यांशों के बीच अंतर की समझ को आसान बनाने के लिए, लेखक अगले खंड में विस्तृत चर्चा के लिए इन्हें तीन भागों में विभाजित किया है।
भाग 1: मृत्यु कारित करने का इरादा
बीएनएस, 2023 की धारा 100 में कहा गया है कि जहां कोई कार्य ‘मौत का कारण बनने’ के इरादे से किया जाता है, वह आपराधिक मानव वध होगा। दिलचस्प बात यह है कि यही प्रावधान धारा 101(a) के तहत पुन: प्रस्तुत किया गया है, जो हत्या से संबंधित है; इसके परिणाम पर बाद में चर्चा की जाएगी। यहां इरादा एक विशेष परिणाम उत्पन्न करने की गहरी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। कोई व्यक्ति कुछ करने के इरादे से कार्य करता है और परिणाम प्राप्त करने की पूर्ण इच्छा के साथ कार्य करता है।
अपराध पर रसेल (12वां संस्करण) के अनुसार,”अपराध में मानसिक तत्व, ‘इरादा’ शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसने एक निश्चित परिणाम लाने का संकल्प लिया है यदि वह संभवतः ऐसा कर सकता है। वह अपने आचरण की रेखा को इस प्रकार आकार देता है कि वह उस विशेष परिणाम को प्राप्त कर सके जिस पर उसका लक्ष्य है।”
कानून मानता है कि एक व्यक्ति अपने कार्यों के स्वाभाविक और अपरिहार्य (इनएविटेबल) परिणामों का इरादा रखता है; इसलिए, जब अभियुक्त का आचरण अन्यथा दिखता है तो उसे ‘इरादे की कमी’ का बचाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि यह प्रदर्शित होता है कि अभियुक्त ने नजदीक से सीधे पीड़ित के सिर में गोली मारी है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एकमात्र इरादा मौत का कारण बनाना था, और अभियुक्त द्वारा इरादे की कमी जैसे किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
‘मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया कार्य’ वाक्यांश को संतुष्ट करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करना होगा:
- आपराधिक कार्य : हमें अभियुक्त के कार्य की जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी इंसान की मौत हुई है।
उदाहरण के लिए: यदि अभियुक्त ने पीड़ित पर गोली चलाई, हालांकि गोली उसे नहीं लगी या केवल उसकी बांह में लगी जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगी और मृत्यु नहीं हुई, तो यह शर्त पूरी नहीं कही जा सकती।
- आपराधिक मनःस्थिति: अभियुक्त के आचरण की जांच करके हमें यह समझना होगा कि क्या अभियुक्त का मौत का कारण बनने का ‘दोषी इरादा’ था। उदाहरण के लिए: यदि अभियुक्त ने पीड़ित के दिल में चाकू मारा था, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उसका इरादा मौत का कारण बनना था।
- आकस्मिकता का तत्व: अभियुक्त के कार्य और मृत्यु के बीच संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्ति की मृत्यु अभियुक्त के कार्य के कारण होनी चाहिए। इस कारणता को मुकदमे में प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए।
उदाहरण के लिए: अभियुक्त ने पीड़ित के भोजन में जहर मिलाया, हालांकि पीड़ित की भोजन को छूने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, अभियुक्त के कार्य और पीड़ित की मृत्यु के बीच कोई आकस्मिकता नहीं है। अत: यह शर्त पूरी नहीं होती। हालांकि यदि पीड़ित ने खाना खाया होता और जहर के कारण उसकी मृत्यु हो गई होती, तो शर्त पूरी हो जाती।
मोती सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963) के मामले में आकस्मिकता के तत्व का पता लगाया गया। 9 फरवरी 1960 को, मृतक को पेट में दो गोली मारी गई थी, जो जीवन के लिए खतरा थी। बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे या नहीं। 1 मार्च 1960 को उनकी मृत्यु हो गई और बिना पोस्टमार्टम के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल इस तथ्य कि बंदूक की गोली जीवन के लिए खतरनाक थी, को यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता कि घटना के तीन सप्ताह से अधिक समय के बाद पीड़ित की मृत्यु, अभियुक्त द्वारा लगी चोटों के कारण हुई थी। अदालत ने आगे कहा कि हत्या के आरोप को साबित करने के लिए यह स्थापित करना जरूरी है कि मृतक की मौत अभियुक्तों द्वारा दी गई चोटों के कारण हुई। चूँकि मौत का कारण स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए अभियुक्त पर आपराधिक मानव वध का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
धारा 100 और धारा 101 (a) दोनों में ‘मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य’ शामिल करने का तर्क
किसी को आश्चर्य होगा कि ‘मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य’ वाक्यांश बीएनएस की धारा 100 और धारा 101 (a) दोनों में क्यों पाया जाता है। समावेशन के तर्क को समझने के लिए, आइए इस कथन को याद करें कि आपराधिक मानव वध जाति है जबकि हत्या प्रजाति है, इसलिए, प्रत्येक कार्य जो प्रजाति का हिस्सा है उसे भी जाति का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने का इरादा रखने वाला कार्य बीएनएस की धारा 101 के अंतर्गत आता है, उसे पहले धारा 100 के अंतर्गत आना होगा। परिणामस्वरूप, प्रत्येक कार्य जो मृत्यु कारित करने के इरादे से किया जाता है और वास्तव में मृत्यु कारित करता है, सीधे तौर पर हत्या के अपराध के अंतर्गत आएगा।
भाग 2: ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मृत्यु होने की संभावना हो
“ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे” के अनुसार, अभियुक्त को ‘शारीरिक चोट’ पहुंचानी चाहिए, जैसे चाकू से वार करना या लोहे की छड़ से चोट पहुंचाना, और यह चोट मौत का कारण बनने की ‘संभावना’ या संभावित (हो सकती है या नहीं भी हो सकती है) होनी चाहिए। इरादा सीधे तौर पर मौत से नहीं बल्कि शारीरिक चोट जो मौत का कारण बन सकती है, से संबंधित है।
- विशेष चोट: इस वाक्यांश को लागू करने के लिए, अभियुक्त का इरादा ‘विशेष’ शारीरिक चोट पहुंचाने का होना चाहिए, जैसे पेट में चाकू मारना आदि। उदाहरण के लिए, यदि A कार चला रहा था और उसने B को मारा, तो यहां कोई विशेष चोट देने का इरादा नहीं था। यह कार्य ‘शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा, जिससे मृत्यु हो सकती है’ वाक्यांश के अंतर्गत नहीं आ सकता क्योंकि यह किसी विशेष चोट का इरादा नहीं था।
- चोट पहुंचाने का इरादा जो वास्तव में पहुंचाई गई है: इसके अतिरिक्त, अभियुक्त का इरादा उस चोट को कारित करने का रहा होगा जो वास्तव में पहुंचाई गई थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरे की बांह पर वार करना चाहता है लेकिन पीड़ित हिल जाता है जिसके कारण वार पीड़ित के सिर पर पड़ता है। यहां, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने उस चोट का इरादा किया था जो वास्तव में पहुंचाई गई थी।
- जानबूझकर की गई चोट से मृत्यु होने की संभावना: शरीर को होने वाली चोट के कारण मौत होने की संभावना चिकित्सीय राय के अनुसार एक वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) जांच है। इसलिए, वास्तव में हुई शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे को साबित करना होता है, यह ज्ञान आवश्यक नहीं है कि ऐसी शारीरिक चोट से व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है।
इसलिए, शरीर पर विशेष चोट पहुंचाने का इरादा एक व्यक्तिपरक (सब्जेक्टिव) जांच है और क्या उस शारीरिक चोट से मृत्यु होने की संभावना थी या नहीं, यह वस्तुनिष्ठ जांच है।
- बाहरी चोट के कारण आंतरिक चोट: जब भी किसी व्यक्ति के मन में किसी बाहरी चोट पहुंचाने का इरादा होता है, तो उसके मन में होने वाली सभी आंतरिक चोटों के इरादे का भी श्रेय दिया जाएगा। चोट की प्रकृति के आधार पर, उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या ऐसी बाहरी और आंतरिक चोट एक साथ ऐसी थी कि जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।
उदाहरण के लिए, यदि A ने पसली वाले क्षेत्र में B को मुक्का मारा है। परिणामस्वरूप, पसलियां टूट गईं और फेफड़े में छेद हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की चोट पहुंचाने का इरादा अभियुक्त पर आरोपित किया जाएगा, और वह यह दावा नहीं कर सकता कि उसका इरादा B के फेफड़े को छेदने का नहीं था।
संक्षेप में, इस वाक्यांश के अनुप्रयोग को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों को पूरा करना होगा:
- विशिष्ट शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा,
- शरीर की चोट जिससे’मौत का कारण बनने की संभावना’ होनी चाहिए।
स्पष्टीकरण 1
बीएनएस, 2023 की धारा 100 का स्पष्टीकरण 1 उस कार्य से संबंधित है जिसमें व्यक्ति सीधे और स्वतंत्र रूप से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं बनता है, बल्कि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु को तेज करता है। इस मामले में, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वह पहले से ही किसी विकार, बीमारी या शारीरिक कमजोरी से पीड़ित है और अभियुक्त के कार्य से पीड़ित की मृत्यु तेज हो जाती है। इसे माना जाएगा कि उसने व्यक्ति की हत्या कर दी है और यह दलील कि यह उसका स्वतंत्र कार्य नहीं था जिसके कारण मृत्यु हुई है, उसके लिए उपलब्ध नहीं होगी।
उदाहरण के लिए: A ने B को पसलियों वाले क्षेत्र में मुक्का मारा, उसकी पसली पहले से ही टूटी हुई थी, जिससे अंततः B की मृत्यु हो गई। A आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी मे नहीं आते है के लिए उत्तरदायी है। भले ही यह साबित हो जाए कि अगर B की पसलियां नहीं टूटी होती, तो वह मुक्के के कारण नहीं मरता। इस मामले में, चूंकि A ने B की मृत्यु को तेज कर दिया है, जो पहले से ही चोट से पीड़ित था, उसे उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।
स्पष्टीकरण 2
बीएनएस, 2023 की धारा 100 के स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि यदि अभियुक्त ने प्रारंभिक शारीरिक चोट पहुंचाई जिससे पीड़ित की मृत्यु हो गई, तो अभियुक्त यह दावा नहीं कर सकता कि पीड़ित उचित चिकित्सा उपचार और देखभाल के साथ बच गया होता।
यहां ‘कॉजा साइन क्वा नॉन’ यानी प्रारंभिक कारण देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, A ने X को पेट में छुरा घोंपा। B X को कंधे पर अस्पताल ले जाता है लेकिन गलती से उसे गिरा देता है। जब वे पहुंचते हैं, तो C, एक कंपाउंडर, ऑपरेशन करता है, लेकिन X की मृत्यु हो जाती है। इस मामले में, A यह तर्क नहीं दे सकता कि अगर उचित उपचार दिया गया होता तो X बच जाता।
यह मूल रूप से उन मामलों को संदर्भित करता है जहां प्राथमिक कारण अभियुक्त द्वारा निर्धारित किया गया है, लेकिन मृत्यु किसी आगामी कारण से होती है। उदाहरण के लिए, यदि A ने B को मामूली चोट पहुंचाई, लेकिन B की मृत्यु गैंग्रीन के कारण हुई, तो A उत्तरदायी होगा क्योंकि प्राथमिक कारण A द्वारा शुरू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप गैंग्रीन हुआ।
सोभा और अन्य बनाम किंग एम्परर (1935)
तथ्य: इस मामले में अभियुक्त ने अपने भाई के साथ मिलकर मृतक से झगड़ा किया। अभियुक्तों ने मृतक के सिर पर लाठी से वार किया और उस पर लात-घूंसे भी बरसाए, लड़ाई के एक सप्ताह के बाद, मृतक की मृत्यु हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि मौत की वजह सेप्सिस इलाज में लापरवाही की वजह से हुआ।
उठाए गये मुद्दे: क्या अभियुक्त का कार्य पीड़िता की मौत का प्राथमिक कारण था?
निर्णय: अवध उच्च न्यायालय ने माना कि मौके पर हुआ हमला एक सामान्य झगड़ा था और लाठी से केवल एक ही वार किया गया था, जिसे डॉक्टरों के अनुसार केवल एक साधारण चोट के रूप में संदर्भित किया गया था। मृत्यु का प्राथमिक कारण सेप्सिस के उपेक्षापूर्ण उपचार है। स्पष्टीकरण में वह स्थिति शामिल है जहां मृत्यु का प्राथमिक कारण अभियुक्त का कार्य है और यदि उसे कुशल उपचार प्रदान किया गया होता तो मृत्यु को रोका जा सकता था। इसमें यह शामिल नहीं है कि चोट के बाद उपेक्षापूर्ण उपचार मृत्यु का प्राथमिक कारण है।
जिससे अभियुक्त को केवल आईपीसी, 1860 के धारा 325 (बीएनएस, 2023 की धारा 116) के तहत दोषी ठहराया गया था, न कि आईपीसी, 1860 की धारा 304 (बीएनएस, 2023 की धारा 105) के तहत।
भाग 3: यह जानते हुए किया गया कार्य कि ऐसे कार्य से उसकी मृत्यु होने की संभावना है
धारा 100 के तीसरे वाक्यांश में कहा गया है कि ‘आपराधिक मानव वध एक ऐसा कार्य है जो इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि ऐसे कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।’ यह वाक्यांश ज्ञान के तत्व से संबंधित है। यहां, “ज्ञान” का तात्पर्य किसी व्यक्ति की तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में जागरूकता या समझ से है। अभियुक्त को पता होना चाहिए कि वह जो कार्य कर रहा है, उससे मृत्यु होने की संभावना है।

वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य (1956) के ऐतिहासिक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालयने इरादे और ज्ञान के बीच अंतर किया। इस मामले में अभियुक्त ने शादी की दावत के दौरान नशे की हालत में 16 साल के लड़के को गोली मार दी। उसने दावा किया कि वह इतना नशे में था कि उसे लड़के को मारने का न तो इरादा था और न ही इसकी जानकारी थी। न्यायालय ने कहा कि,“ज्ञान किसी कार्य के परिणामों की जागरूकता है। कई मामलों में, इरादा और ज्ञान एक-दूसरे में विलीन हो जाते हैं और कमोबेश एक ही अर्थ रखते हैं, और इरादे को ज्ञान से अनुमान लगाया जा सकता है। ज्ञान और इरादे के बीच की रेखा निस्संदेह पतली है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि वे अलग-अलग चीजें हैं।”
“शब्द ‘संभावित’ का अर्थ है ‘शायद’ और इसे ‘निश्चित रूप से’ से अलग किया जाता है। जब किसी घटना के होने की संभावना उसके न होने की संभावना के बराबर या अधिक होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह घटना ‘संभावित’ है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या अभियुक्त को अपने कार्य से मृत्यु होने की संभावना का ज्ञान था। इसका परीक्षण एक उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यदि कोई उचित व्यक्ति अभियुक्त की स्थिति में होता तो क्या उसे मृत्यु कारित करने की संभावना के बारे में पता होता? यदि हां, तो वही ज्ञान अभियुक्त पर आरोपित किया जाएगा।
उदाहरण के लिए: यदि एक छोटे से कमरे में 10 लोग मौजूद हैं और अभियुक्त ने छत की ओर गोली चलाई है, तो यहां किसी भी समझदार व्यक्ति को यह ज्ञान होगा कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।
संक्षेप में, इस वाक्यांश के अनुसार किसी कार्य को आपराधिक मानव वध मानने के लिए दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- सबसे पहले, कार्य या अवैध चूक अपराधी द्वारा की जानी चाहिए।
- दूसरा, अपराधी के बारे में यह ज्ञान कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।
स्पष्टीकरण 3
बीएनएस, 2023 की धारा 100 के स्पष्टीकरण 3 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किए गये कार्य से किस बच्चे की मृत्यु हो जाती है जो अभी मां के गर्भ में है, उस कार्य को आपराधिक मानव वध नहीं माना जाएगा। यदि इस की सभी तत्व पूरे होते है।
यदि बच्चे का कोई हिस्सा बाहर आ चुका है, भले ही बच्चा पूरी तरह से पैदा न हुआ हो, और यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वह आपराधिक मानव वध के अपराध के अंतर्गत आएगा। हालांकि, यदि बच्चा पूरी तरह से गर्भ में है, तो वह आपराधिक मानव वध के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा।
बीएनएस, 2023 की धारा 100 पर आधारित मामले
शनमुगम @ कुलंदावेलु बनाम तमिलनाडु राज्य (2002)
तथ्य
इस मामले के तथ्यों के अनुसार उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को, पीड़ित बोरवेल से पानी लाने के लिए अपने खेतों में गया, जहां उसने अपने बड़े भाई को ऐसी जगह पर सीटी बजाते हुए देखा, जहां अक्सर महिलाएं आती थीं। उन्होंने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी देर के झगड़े के बाद अभियुक्त अपनी झोपड़ी की ओर भागा और हथियार लेकर बाहर आया। वह पीड़ित पर झपटा और उसके पेट और सीने में चाकू घोंप दिया।
उठाए गये मुद्दे
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या पीड़ित पर पाई गई चोटें प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, ताकि आईपीसी, 1860 की धारा 300 (बीएनएस, 2023 की धारा 101) के दायरे में आ सकें।
निर्णय
न्यायालय ने माना कि डॉक्टर की राय के अनुसार, चाकू का वार किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर नहीं था क्योंकि पेट के अंदर कोई चोट नहीं थी। यह कहा गया कि मौत संक्रमण के कारण सेप्टिसेमिया के परिणामस्वरूप हुई। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि पित्ताशय (गॉलब्लैडर) में चाकू के घाव के कारण मृत्यु निश्चित थी।
इन तथ्यों के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त की ओर से मृत्यु के इरादा से नहीं बचा जा सकता, और इस प्रकार यह मामला ऐसा था, जहां चोटें ऐसी प्रकृति की थी कि वे मृत्यु का कारण बन सकती थीं। इसके अलावा, अभियुक्त ने ऐसी चोटें पहुंचाने का इरादा किया और वास्तव में ऐसी चोटें पहुंचाई, इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 299 (बीएनएस, 2023 की धारा 100) के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था, और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के पहले भाग (बीएनएस, 2023 की धारा 105 के पहले भाग) के तहत दंडनीय ठहराया गया।
राजन बनाम गोमंगलम पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, अब तिरुपुर जिला के पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत राज्य, (2016)
तथ्य
इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: अभियुक्त पीड़िता का पति था; उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अभियुक्त पति, जो शराबी बन गया था, उसने अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। मृतक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दंपति के बीच झगड़ा हुआ। अभियुक्त ने गुस्से में आकर मृतिका का मुंह और नाक बंद कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। अभियुक्त ने यह मानते हुए कि वह मर गई है, उसे चटाई पर लिटा दिया, उस पर मिट्टी का तेल डाला, आग लगा दी और घर को अंदर से बंद कर दिया।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 (बीएनएस, 2023 की धारा 103) के तहत हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है?
निर्णय
मद्रास उच्च न्यायालय ने विश्लेषण किया कि जब अभियुक्त ने मृतक को थप्पड़ मारने का पहला कार्य किया, तो उसका मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था जो मृत्यु का कारण बन सके। जब उसने मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का दूसरा कार्य किया, तो उसका मृतक की मृत्यु या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था जो मृत्यु का कारण बन सके।
अदालत ने माना कि ये दोनों कार्य एक ही कार्य का गठन करते हैं, और अभियुक्त का किसी भी बिंदु पर मृत्यु या शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। वह धारा 299 ( बीएनएस, 2023 की धारा 100) के पहले या दूसरे भाग के अंतर्गत नहीं आएगा। चूंकि दूसरा कार्य, मिट्टी का तेल डालना और आग लगाना, पर्याप्त देखभाल और ध्यान दिए बिना किया गया था, और लापरवाही से किया गया था, बिना यह सत्यापित किए कि मृतक जीवित है या नहीं, अदालत ने उस पर ज्ञान आरोपित किया जैसा कि धारा 299 (बीएनएस, 2023 की धारा 100) के तीसरे भाग के तहत आवश्यक है और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दूसरे पैराग्राफ (बीएनएस, 2023 की धारा 105 ) के तहत दंडित किया गया था।
कपूर सिंह बनाम पेप्सू राज्य (1954)
तथ्य
इस मामले में तथ्य इस प्रकार हैं: घटना से एक वर्ष पहले, मृतक के बेटे ने अपीलकर्ता के बेटे के पैर पर गंभीर चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसका पैर काटना पड़ा। दुर्घटना के कारण, अपीलकर्ता को पिता और पुत्र के प्रति द्वेष था और वह बदला लेने की कोशिश कर रहा था। 30 सितंबर 1952 के दिन, अपीलकर्ता मृतक से मिला और उसने और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया, और अभियुक्त ने एक मोटी लकड़ी की छड़ी से मृतक के हाथ और पैरों पर 18 चोटें पहुंचाईं।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 (बीएनएस, 2023 की धारा 103) के तहत हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है?
निर्णय
अदालत ने विश्लेषण किया कि, हालांकि चोटों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनमें से कोई भी शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं थी। शीर्ष अदालत ने माना कि अपीलकर्ता का मकसद प्रतिशोध लेना था और इस तरह उसने मृतक के केवल हाथ और पैर पर चोटें पहुंचाईं और शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कोई चोट नहीं पहुंचाई। इससे साफ जाहिर होता है कि उसका इरादा मृतक की हत्या करने का नहीं था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि चोटें मृतक की मृत्यु का कारण बनने के इरादे से पहुंचाई गई थीं। हालाँकि, इतनी शारीरिक चोटें थीं कि उन्हें पता था कि इससे मृतक की मृत्यु होने की संभावना होगी। इसलिए, अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 299 (बीएनएस, 2023 की धारा 100) के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बीएनएस, 2023 की धारा 105 के तहत आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी मे नहीं आते है उनके लिए सजा
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105 (जो पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 थी) आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, जैसा कि बीएनएस, 2023 की धारा 100 में परिभाषित किया गया है के लिए सजा का प्रावधान करती है।
बीएनएस, 2023 की धारा 105 में कहा गया है कि यदि अभियुक्त का कार्य बीएनएस, 2023 की धारा 100 के पहले या दूसरे भाग के अंतर्गत आता है, जो कि मृत्यु का कारण बनने के इरादे या मृत्यु की संभावना वाली शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से संबंधित है, तो अभियुक्त को आजीवन कारावास या न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
दूसरा भाग उस स्थिति में सजा से संबंधित है जब अभियुक्त का कार्य बीएनएस, 2023 की धारा 100 के तीसरे भाग के अंतर्गत आता है, जो अभियुक्त की ओर से इस ज्ञान से संबंधित है कि उसके कार्य से मृत्यु होने की संभावना है, तो ऐसे मामले में जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।
अंबाजगन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व (2023)
तथ्य
इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं: मृतक और अभियुक्त दोनों कृषक थे, जिनके पास आस-पास के खेत थे। खेतों के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। रास्ते के इस्तेमाल को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। अभियुक्त ने गुस्से में आकर मृतक के सिर पर कुदाल, जो एक कृषि उपकरण है, से वार कर दिया। जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त को आईपीसी की धारा 302 (बीएनएस, 2023 की धारा 103) के तहत हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह नहीं कहा जा सकता कि जब अपीलकर्ता ने हथियार से मृतक को मारा, तो उसका इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जो सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो, पोस्ट-परीक्षण रिपोर्ट में दिखाई गई चोटें वास्तव में पार्श्विका(पेरिएटल) हड्डी और टेम्पोरल हड्डी टूट गई हैं और चोट वास्तव में मृत्यु का कारण थी। हालांकि, मुख्य प्रश्न यह है कि क्या यह अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता का इरादा ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का था जो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। अदालत ने माना कि अपीलकर्ता को केवल इस ज्ञान के साथ जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि यह ऐसी चोट का कारण बनने की संभावना थी जो मृत्यु का कारण बन सकती थी।
अदालत ने आगे आईपीसी की धारा 304 के दो पैराग्राफों के बीच अंतर को स्पष्ट किया है- यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति का कार्य ‘मृत्यु का कारण बनने की संभावना वाली शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे’ के अंतर्गत आता है, तो यह धारा 304 के पहले पैराग्राफ (बीएनएस, 2023 की धारा 105 के पहले पैराग्राफ) के तहत दंडनीय है। हालांकि, यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि ‘मृत्यु का कारण बनने की संभावना है’, तो यह धारा 304 के दूसरे पैराग्राफ (बीएनएस, 2023 की धारा 105 के दूसरे पैराग्राफ) के तहत दंडनीय है। इसलिए, प्रभाव में, इस धारा का पहला पैराग्राफ तब लागू होगा जब ‘अपराधपूर्ण इरादा’ हो, जबकि दूसरा पैराग्राफ तब लागू होगा जब ऐसा कोई इरादा न हो लेकिन ‘अपराधपूर्ण ज्ञान’ हो।

एलिस्टर एंथोनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012)
तथ्य
इस मामले में 12 नवंबर 2006 को, मुंबई शहर में सुबह-सुबह एक कार फुटपाथ से टकरा गई और फुटपाथ पर सो रहे सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चिकित्सीय साक्ष्य से घटना के समय अभियुक्त के खून में अल्कोहल की मौजूदगी सिद्ध की गई। उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 299 के तहत आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी में नहीं आते है, के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और धारा 304 के दूसरे पैराग्राफ के तहत दंडित किया गया।
उठाए गये मुद्दे
क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 304 के दूसरे पैराग्राफ के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को दी गई सजा में कोई संशोधन आवश्यक है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निष्कर्ष को सही ठहराया कि घटना के समय अभियुक्त शराब के प्रभाव में था और उसने इस हालत में अपनी कार बहुत तेज गति से चलाकर सात लोगों की जान ले ली। उसे इस ज्ञान के साथ आरोपित किया गया है कि उसके कार्य इन परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बन सकते थे। उच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी और कहा गया था कि अभियुक्त को धारा 304 के दूसरे पैराग्राफ के तहत दंडित करने के लिए अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि मृत्यु अभियुक्त के कार्य के कारण हुई थी और उसे पता था कि उसका कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है।
बीएनएस, 2023 की धारा 101 (आईपीसी, 1860 की धारा 300) के तहत आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी मे आते है
यह धारा कहती है कि आपराधिक मानव वध हत्या है; यह इस तथ्य को प्रतिबिंबित करता है कि किसी कार्य को हत्या मानने के लिए सबसे पहले उसे आपराधिक मानव वध होना चाहिए। यह हत्या नहीं हो सकती इसलिए यह अंतर्निहित है कि आपराधिक मानव वध जाति है और हत्या प्रजाति है।
बीएनएस, 2023 की धारा 101 की शुरुआत ‘इसके बाद अपवादित मामलों को छोड़कर’ शब्दों से होती है, आपराधिक मानव वध हत्या है। यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि यदि धारा 101 के पांच अपवादों में से कोई भी लागू होता है, तो आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होगी। इसलिए, आपराधिक मानव वध के किसी कार्य को हत्या के बराबर होने के लिए, या तो बाद के भागों में से किसी एक को लागू किया जाना चाहिए और कोई भी अपवाद लागू नहीं होना चाहिए।
मौत कारित करने का इरादा
धारा 101(a), धारा 100 के पहले भाग के समान है, जो एक ऐसे कार्य से संबंधित है जो मौत का कारण बनने के इरादे से किया जाता है। ‘आपराधिक मानव वध हत्या है’ कथन को सही ठहराने के लिए, सबसे पहले इस कार्य को आपराधिक मानव वध की परिभाषा के अंतर्गत आना होगा। इसलिए, हम धारा 100 के तहत पहले भाग को धारा 101(a) के समान पाते हैं। वास्तव में, मौत का हर जानबूझकर किया गया कारण धारा 101 के तहत हत्या के अंतर्गत आता है, धारा के पहले भाग के अंतर्गत आने वाली कोई भी चीज़ स्वचालित रूप से सीधे धारा 101 (a) के अंतर्गत आ जाएगी। दोनों प्रावधानों का निहितार्थ और दायरा एक समान है। इरादा कम या अधिक डिग्री का नहीं हो सकता है, इसलिए इरादे की समान डिग्री दोनों धाराओं में पाई जाती है।
इरादे का अर्थ है किसी परिणाम को उत्पन्न करने की इच्छा; कोई आकस्मिक आचरण नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इस धारा के लिए एक निश्चित आचरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के माथे के बीच से करीब से बंदूक से गोली चलाना स्पष्ट रूप से अभियुक्त के मृत्यु का कारण बनने के इरादे को प्रकट करता है।
इरादा हमेशा मन की एक अवस्था होती है और इसे केवल इसकी बाहरी अभिव्यक्तियों से ही सिद्ध किया जा सकता है। जहां शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर तेज धार वाले उपकरणों से चोट पहुंचाई जाती है, वहां मारने का इरादा अपराधी का माना जा सकता है, जैसा कि चाहत खान बनाम हरियाणा राज्य (1972) में कहा गया है।
वसंत बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) के मामले में अभियुक्त और मृतक के बीच कुछ पुरानी दुश्मनी थी और उनके बीच थोड़ी हाथापाई भी हुई थी, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने शांत कर दिया था। इसके बाद अभियुक्त अपनी जीप के पास गया और उसे तेज गति से मृतक की ओर गलत दिशा में ले गया और उसे नीचे गिरा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। जिससे यह साबित हो गया कि अभियुक्त द्वारा गलत दिशा में जीप चलाने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उसका कार्य स्पष्ट रूप से मृतक की मृत्यु का कारण बनने का उसका इरादा दर्शाता है।
मौत का कारण बनने के इरादे की जांच की जानी चाहिए। यह देखना होगा कि अभियुक्त निश्चितता के साथ परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अधिक निश्चितता के साथ कार्य करता है। व्यक्ति के आचरण से उसकी मंशा की जांच की जाती है। उसने यह कार्य कैसे किया? आचरण साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जाता है और फिर एक उचित व्यक्ति के अनुसार उसके इरादे को समझने के लिए उसी आचरण की जांच की जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि एक उचित व्यक्ति ने अभियुक्त के समान कार्य किया होता तो उसका इरादा क्या होता?
उदाहरण के लिए, यदि A किसी वयस्क व्यक्ति के सिर पर एक बार छड़ी से वार करता है, तो यह कार्य मृत्यु कारित करने के उसके इरादे को प्रकट नहीं करता है। हालांकि, यदि वह दो महीने के बच्चे के सिर पर उसी छड़ी से एक ही वार करता है, तो यह मौत का कारण बनने का इरादा प्रकट कर सकता है।
ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिसके कारण अपराधी को पता हो कि इससे मृत्यु होने की संभावना है
धारा 101(b) में कहा गया है कि जब कोई कार्य ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है, जिसके बारे में अपराधी जानता है कि जिसे नुकसान पहुंचाया गया है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो यह हत्या की श्रेणी में आएगा।
ज्ञान शब्द के साथ संभाव्य शब्द मृत्यु की निश्चितता का सूचक है न कि संभावना का। यह बताता है कि किसी चीज़ के घटित होने की संभावना बहुत अधिक है।
धारा 100 (b) के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं-
- शारीरिक चोट लग जाती है
- अपराधी को व्यक्तिपरक ज्ञान है कि विशिष्ट शारीरिक चोट से उस विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिसे यह चोट लगी है
- आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी मे आते है, उसमे विशिष्ट परिस्थिति के ज्ञान की आवश्यकता एक अतिरिक्त तत्व है।
हालांकि धारा 100 और धारा 101 में एक विशिष्ट शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे और उस विशेष शारीरिक चोट के मृत्यु का कारण बनने की संभावना आम है, बाद वाले में अभियुक्त के इस विशिष्ट ज्ञान का अतिरिक्त तत्व आवश्यक है कि शारीरिक चोट उस विशेष पीड़ित की मृत्यु का कारण बन सकती है।
यह खंड ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां अपराधी को विशिष्ट स्थिति या विशेष पीड़ित की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विशेष ज्ञान होता है जिसके कारण उसकी जानबूझकर शारीरिक चोटें घातक होने की संभावना होती है जैसा कि अंडा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (1966) मे कहा गया है।
उदाहरण के लिए, यदि पीड़ित की तिल्ली (स्प्लीन) में सूजन है और अभियुक्त को इसकी विशेष जानकारी है, यदि तो वह पीड़ित को उस विशेष स्थान पर मारता है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो धारा 100 के दूसरे भाग के प्रयोजन के लिए, उसका इरादा था उस चोट का कारण बनें और डॉक्टर की राय के अनुसार उस विशेष चोट के कारण मृत्यु होने की संभावना थी। हालांकि, उसके कार्य को धारा 101 के तहत लाने के लिए, अतिरिक्त आवश्यकता है कि अपराधी को सूजी हुई तिल्ली के बारे में विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए जो यहाँ मौजूद है और इस प्रकार, यह उसके कार्य को धारा 101 के तहत लाएगा जो कि हत्या है।
प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त शारीरिक क्षति पहुँचाने का इरादा
धारा 101 (c) के अनुसार, अभियुक्त का इरादा शारीरिक चोट पहुंचाने का होना चाहिए और जो शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा है, वह “प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त” होना चाहिए।
धारा 101(c) धारा 100 के तहत पाए जाने वाले ‘मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट’ वाक्यांश का तीव्र रूप है। किसी कार्य को धारा 101(c) के अंतर्गत आने के लिए, यह सामान्य कारण प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। धारा 100 और धारा 101(c) के बीच मृत्यु की संभावना की डिग्री में अंतर है।
धारा 101 (b) द्वारा दो-चरणीय परीक्षा की परिकल्पना की गई है –
- शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे का मतलब यह है कि जो शारीरिक चोट पहुंचाई गई वह बिल्कुल वही चोट थी जिसे अभियुक्त पहुंचाना चाहता था। यह अभियुक्त के दिमाग का व्यक्तिपरक परीक्षण है,
- इच्छित शारीरिक चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य कारणों से पर्याप्त होनी चाहिए। यह वस्तुनिष्ठ पाठ है, जो डॉक्टरों की राय पर आधारित है। इस तत्व को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त के दिमाग की जांच नहीं की जानी चाहिए।
बीएनएस, 2023 की धारा 101(c) पर मामले
विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958)
तथ्य
इस मामले में अभियुक्त ने पीड़ित के पेट पर भाले से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
उठाए गये मुद्दे
क्या सामान्य प्रक्रिया में अभियुक्त द्वारा किया गया वार मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 300, (तीसरा) (बीएनएस, 2023 की धारा 101(c)) के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि पीड़ित पर पाई गई शारीरिक चोट वास्तव में अभियुक्त द्वारा इरादा से किया गया था। इसके अलावा, यह जांचना होगा कि क्या उक्त इरादा शारीरिक चोट सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। बाद की जांच चिकित्सा राय पर आधारित है। यदि उपरोक्त दोनों तत्वों को स्वीकृत किया जाता है, तो आपराधिक मानव वध हत्या के बराबर होगी। दूसरे शब्दों में, “सवाल यह नहीं है कि कैदी का इरादा कोई गंभीर चोट पहुंचाने का था या मामूली चोट पहुंचाने का, बल्कि सवाल यह है कि क्या उसका इरादा ऐसी चोट पहुंचाने का था जो मौजूदा समय में साबित हो चुकी है…. जहां तक इरादे का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि उसका इरादा मारने का था या किसी खास गंभीरता की चोट पहुंचाने का, बल्कि यह है कि क्या उसका इरादा विचाराधीन चोट पहुंचाने का था”।
चूंकि भाला का वार ऐसा था कि “यह आंतों में प्रवेश कर गया और आंतों के तीन कुंडलियाँ (कोइल्स) घाव से बाहर आ गए और पचा हुआ भोजन फटी तीन जगहों से निकल गया।” अदालत ने अंततः हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया।
इंदर सिंह बग्गा सिंह बनाम पेप्सू राज्य (1954)
तथ्य
इस मामले के तथ्य यह थे कि मृतक पीड़िता ने अपीलकर्ता की भाभी के प्रति पहले कदम बढ़ाया था। अपीलकर्ता ने उसे भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद, उनके गांव में शादी थी, मृतक अभियुक्त के घर के सामने खड़ा था और एक पीरे सिंह नामक व्यक्ति के साथ बातचीत में लगा हुआ था। उस समय, अभियुक्त अपने घर से लाठी लेकर दौड़ा और पीछे से पीड़ित के सिर पर एक वार किया, और जब वह मुड़ा, तो उसके सिर पर एक और वार किया गया। मृतक के जमीन पर गिरने के बाद भी, अपीलकर्ता ने उसकी गर्दन पर एक और वार किया, कुल मिलाकर छह वार किए गए। जब आस-पास के लोगों ने शोर मचाया, तो अपीलकर्ता भाग गया। कुछ दिनों बाद, पीड़ित की मृत्यु मस्तिष्क के संपीड़न (कम्प्रेशन) के कारण हो गई।
उठाए गये मुद्दे
अभियुक्त ने क्या अपराध किया है और उसे क्या सजा दी जानी चाहिए?
निर्णय
डॉक्टर की राय के अनुसार, यह कहा गया कि पहली चोट एक घातक चोट थी जिसके कारण उनके मस्तिष्क में संपीड़न के लक्षण विकसित हुए, जो धीरे-धीरे बढ़ते गए, उन्होंने कहा कि यह चोट प्रकृति की सामान्य शक्ति के कारण होने वाली मौत के लिए पर्याप्त थी।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि वार अभियुक्त द्वारा किया गया था जिससे पीड़ित की मृत्यु हुई, लेकिन इस्तेमाल किया गया हथियार लाठी था न कि लोहे की छड़। इसके अलावा, मृतक मजबूत कद काठी का एक युवा व्यक्ति था और अभियुक्त को उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से काम करने वाला नहीं माना जा सकता था। चिकित्सा साक्ष्य के बावजूद, अदालत का मानना था कि चोट सामान्य कारण प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि वह चोट लगने के तीन सप्ताह बाद तक जीवित रहा, जिससे उसे आईपीसी की धारा 299 (बीएनएस की धारा 100) के तहत ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया गया और आईपीसी की धारा 304 (बीएनएस की धारा 105) के पहले पैराग्राफ के तहत दंडनीय है।
आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायावारापु पुन्नय्या और अन्य (1976)
तथ्य
इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे, एक दिन मृतक अन्य दो लोगों के साथ एक गंतव्य (डेस्टिनेशन) के लिए बस में चढ़ा। बाद में अभियुक्त अन्य लोगों के साथ बस में चढ़े। जब मृतक और उसके साथी बस से उतरे, तो उनका पीछा पांच अभियुक्तों ने किया। मृतक और अभियुक्त के बीच राजनीतिक विवाद था और मृतक ने पिछले दिन अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उस दिन वह उसी के संबंध में पुलिस थाने जा रहा था। दो अभियुक्तों ने भारी लाठियां उठाईं और मृतक के पीछे गए, जो एक वृद्ध व्यक्ति था और भागने में असमर्थ था। उसने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, अभियुक्तों ने मृतक के पैरों और हाथों को पीटा और उसे बेहोश होने तक पीटते रहे। इसके बाद वे चले गए। डॉक्टर की राय के अनुसार, मृतक पर कुल 19 चोटें थीं, जिनमें से नौ गंभीर थीं, और अगली सुबह सदमे और रक्तस्राव (हैमरेज) के कारण उसकी मृत्यु हो गई, चोटें संचयी रूप से सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त हत्या के अपराध का दोषी है?
निर्णय
न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए दो तत्वों की जांच करनी होगी। सबसे पहले, जिस कार्य के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई वह अभियुक्त द्वारा किया गया था, अर्थात, मृत्यु स्पष्ट रूप से अभियुक्त के कार्यों की श्रृंखला से संबंधित हो सकती है।
दूसरा, आपराधिक मनःस्थिति के तत्व की जांच अभियुक्त के आचरण से की जाती है। सभी चोटें पैरों और बांहों पर दी गई है, शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर कोई वार नहीं किया गया। इसलिए मृत व्यक्ति को मारने का सीधा इरादा संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, सबूतों से यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तों का इरादा उन शारीरिक चोटों को कारित करने का था जो वास्तव में पाई गई थीं और उनका इरादा और ज्ञान रहा होगा कि ऐसी शारीरिक चोटों से मृत्यु होने की संभावना थी। इसलिए, आपराधिक मानव वध किसी भी संदेह से परे है।
इसके अलावा इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या आपराधिक मानव वध हत्या के समान है, इस कार्य की जांच आईपीसी की धारा 300 (बीएनएस, 2023 की धारा 101 (c)) के तहत की जानी चाहिए। धारा के अनुप्रयोग के लिए दो तत्वों पर चर्चा करनी होगी। सबसे पहले, क्या मृतक पर पाई गई शारीरिक चोटें अभियुक्त द्वारा जानबूझकर पहुंचाई गई थीं, जो एक व्यक्तिपरक जांच है। दूसरे, क्या ये चोटें प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं, जो एक वस्तुनिष्ठ जांच है। ये दोनों कारक मामले में साबित हो गए हैं और इस तरह अभियुक्त को हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

हरजिनदर सिंह अलियास जिंडा बनाम दिल्ली प्रशासन (1967)
तथ्य
इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि 31 जनवरी 1962 को दलीप कुमार और अपीलकर्ता के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई में अपीलकर्ता हार गया, परिणामस्वरूप वह दलीप कुमार को धमकी देकर चला गया। अपीलकर्ता एक अन्य के साथ दलीप कुमार के घर पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। इस समय दलीप सिंह के भाई केवल कुमार ने हस्तक्षेप किया। उस समय अभियुक्त के साथ आए व्यक्ति ने दलीप सिंह को पकड़ लिया और अपीलकर्ता ने उसकी जांघ के ऊपरी हिस्से पर चाकू से वार कर दिया।
चाकू से किए गए वार के कारण ऊरु धमनी (फेमरल आर्टेरी) और नस कट गई, जिससे मांसपेशियों में और बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से के आसपास रक्त का संलयन (फ्यूज़न) हो गया, जिससे काफी खून बह गया। डॉक्टरों के अनुसार, इन वाहिकाओं (वेसल्स) को काटने से आघात और रक्तस्राव के कारण तत्काल मृत्यु हो सकती है।
उठाए गये मुद्दे
क्या धारा 300 के तीसरे चरण के अनुप्रयोग की आवश्यकताएं सिद्ध हो गई हैं?
निर्णय
अभियोजन ने तर्क दिया कि वीरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में वर्णित सभी तत्व पूरे हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह देखा गया कि:
सबसे पहले यह निष्पक्ष रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि शारीरिक चोटें मौजूद हैं।
दूसरा, चोट की प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए।
तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष चोट को पहुंचाने का इरादा था और यह चोट आकस्मिक या अनजाने में नहीं थी या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा नहीं था।
एक बार जब ये सभी तत्व मौजूद हो जाते हैं, तो जांच यह जांचने के लिए आगे बढ़ती है कि ऊपर वर्णित प्रकार की चोट, जो तीन तत्वों से बनी है, प्रकृति के सामान्य कारण से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। यह जांच वस्तुनिष्ठ है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।
सवाल यह है कि क्या अभियुक्त का इरादा पीड़ित को विशेष चोट पहुंचाने का था। यदि वह यह दिखाने में सक्षम है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, तो धारा के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक इरादा पर्याप्त नहीं है। इस मामले में, परिस्थितियों से पता चलता है कि अभियुक्त का इरादा जांघ के विशेष हिस्से पर चोट पहुंचाने का नहीं था, और चूंकि मृतक लड़ाई के बीच हस्तक्षेप करने और दोनों को अलग करने के लिए झुकने की स्थिति में था, इसलिए चाकू उसकी जांघ पर लगा। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उसने उस विशेष बिंदु पर यह जानते हुए प्रहार किया था कि इससे धमनी कट जाएगी। इसलिए, आईपीसी की धारा 300, तीसरा (बीएनएस, 2023 की धारा 101 (c)) को लागू नहीं किया जा सकता है।
फिर भी, चाकू एक खतरनाक हथियार था, और जब मृतक पर चाकू से वार किया गया था, तो अभियुक्त को पता होगा कि यह शरीर के एक कमजोर हिस्से के पास लगेगा और इससे उसकी मृत्यु होने की संभावना थी। इसलिए, शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मृत्यु होने की संभावना है, इस कार्य को आईपीसी की धारा 299 (बीएनएस, 2023 की धारा 100) के दूसरे भाग के अनुसार स्थापित किया गया है।
किसी आसन्न खतरनाक कार्य के बारे में ज्ञान
धारा 101(d) के अनुसार, किसी कार्य को आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी मे आते है, ऐसा मानने के लिए, कार्य ऐसा होना चाहिए कि अभियुक्त को पता हो कि यह “इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि पूरी संभावना है कि इससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति हो सकती है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो”। इसके अलावा, यह कार्य मृत्यु या ऐसी चोट का जोखिम उठाने के किसी बहाने के बिना किया जाना चाहिए।
इस खंड में तीन आवश्यक तत्व हैं-
- यह ज्ञान कि यह कार्य आसन्न रूप से खतरनाक है
- पूरी संभावना है कि यह कार्य ऐसी शारीरिक चोट का कारण बने जिससे मृत्यु होने की संभावना हो
- यह कार्य जोखिम उठाने के लिए बिना किसी बहाने के किया जाता है
जबकि धारा 100 में, जो जाति है, वहा ‘मृत्यु का कारण बनने की संभावना का ज्ञान’ होने की आवश्यकता होती है, जबकि धारा 101 (d) जो प्रजाति है मे आवश्यक ज्ञान उच्च स्तर (डिग्री) का है। बाद वाले को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है कि कार्य आसन्न रूप से खतरनाक है और सभी संभावना में मृत्यु का कारण बनना चाहिए।
यहाँ, आसन्न का अर्थ है तुरंत या लगभग, निश्चित रूप से घटित होने वाला।
उदाहरण के लिए, A भीड़ में बेतरतीब (रैंडमली) ढंग से गोली चलाता है। उसका लक्ष्य किसी खास हिस्से को निशाना बनाना नहीं है, इसलिए मौत का कारण बनने या शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई सीधा इरादा नहीं है। हालांकि, ऐसी जानकारी है कि इस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है। हालांकि, यदि वह 5-6 गोलियाँ चलाता है तो उसका कार्य धारा 101 (d) के अंतर्गत आएगा।
दूसरे उदाहरण में, यदि A किसी अस्पताल में जाता है और तीन मिनट के लिए टाइम बम लगाता है, तो वह सभी को बम के बारे में बताता है। हम मौत का कारण बनने के सीधे इरादे का आरोप लगाने में सक्षम नहीं हो सकते क्योंकि अभी भी बचने का समय है। चूंकि किसी विशेष शारीरिक चोट का इरादा नहीं है, इसलिए धारा 100 का दूसरा भाग भी लागू नहीं होगा। हालांकि, उसे ऐसा ज्ञान है जिससे मृत्यु होने की संभावना है। फिर हम आगे जांचते हैं कि क्या यह कार्य इतना खतरनाक है कि इसके कारण मृत्यु होने की पूरी संभावना है, यदि उत्तर सकारात्मक है तो यह कार्य धारा 101 (d) के अंतर्गत आएगा।
यह धारा स्वयं ऐसी स्थिति प्रस्तुत करती है जहां आपराधिक मानव वध का कार्य हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में, यदि अभियुक्त के पास जोखिम उठाने का कोई बहाना है, तो धारा 101 (d) लागू नहीं होगी।
बीएनएस, 2023 की धारा 101(d) पर मामले
एंपरर बनाम माउंट धिराजिया (1940)
तथ्य
इस मामले में अपीलकर्ता का पति क्रूर स्वभाव का था और वह अपीलकर्ता को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। अपीलकर्ता अपने गोंद मे अपना बच्चा लेकर भाग रही थी, और खुद को बचाने के लिए अपीलकर्ता कुएं में कूद गई, जिससे बच्चे की मौत हो गई।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त को हत्या के अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है?
निर्णय
यहां अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि, जब अपीलकर्ता कुएं में कूदी, तो उसे पता था कि उसका कार्य आसन्न खतरनाक था, और पूरी संभावना है कि इससे मौत हो सकती है। हालांकि, उसने दावा किया कि जब उसका पति उसका पीछा कर रहा था तो वह घबरा गई थी, इसलिए उसने कुएं में छलांग लगा दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुएं में कूदने का जोखिम उठाने के उसके बहाने पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि उसका कार्य आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, हत्या की श्रेणी में नहीं, क्योंकि उसका पति उसका पीछा कर रहा था, और यह एक दहशत की स्थिति थी जहां उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं था।
ग्यारसीबाई पत्नी जगन्नाथ बनाम मध्य भारत राज्य (1952)
तथ्य
इस मामले में अपीलकर्ता-पत्नी के पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी जिसके कारण वह अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर चली गई। पति उसका पीछा नहीं कर रहा था, इसके बावजूद वह भागकर कुएं में कूद गयी, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गयी।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है?
निर्णय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि कोई आसन्न खतरा नहीं था और इस तरह उसके पास मृत्यु का कारण बनने के जोखिम को उठाने का कोई उचित बहाना नहीं था। इसलिए, उसे हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया गया और उसे आईपीसी की धारा 300 (चौथे) (बीएनएस, 2023 की धारा 101 (d)) के तहत प्रदान किए गए अपवाद का लाभ नहीं दिया गया।
बीएनएस, 2023 की धारा 101 (आईपीसी, 1860 की धारा 300) पर ऐतिहासिक मामले
लक्ष्मण बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2006)
तथ्य
इस मामले में मृतक अन्य लोगों के साथ अनाज लेने गाड़ाघाट गया था और वापस आ रहा था तभी यह घटना घटी। वापस लौटते समय अभियुक्त ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्हें रोका और उन पर तीर और पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। अभियुक्त द्वारा चलाया गया एक तीर मृतक को लगा। चोट लगने पर मृतक गिर गया और तुरंत मर गया।
उठाए गये मुद्दे
न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि प्रयोग किया जाने वाला उचित प्रावधान क्या है?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तथ्य बताते हैं कि तीर दूर से चलाये जा रहे थे, किसी विशेष सटीकता से नहीं। कई तीरों में से एक तीर मृतक को लगा। इसके अलावा, हमले से पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अदालत ने कहा कि स्थापित तथ्य केवल आपराधिक मानव वध का अपराध साबित करते हैं और धारा 304 प्रथम पैरा (बीएनएस की धारा 105) के तहत दंडनीय है।
मनोज कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018)
तथ्य
इस मामले में अभियुक्त और मृतक के बीच कुछ जमीन के स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा लंबित था। घटना उस वक्त हुई जब मृतक विवादित जमीन से लौट रहा था और अभियुक्त बगल के खेत में धान की रोपाई में व्यस्त थे। जब अभियुक्तों ने मृतक को उनकी जमीन पार करते हुए देखा, तो अभियुक्तों में से एक व्यक्ति अचानक आया और मृतक के साथ झगड़ा करने लगा और फिर बाद में अभियुक्त के परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हो गए। झगड़ा बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया और अभियुक्त व अन्य लोगों ने मृतक पर हमला कर दिया। किसी ने चाकू से हमला किया तो किसी ने लाठी से। अपनी जान बचाने के लिए मृतक और अन्य साथियों ने मौके से भागने का प्रयास किया। हालांकि, बाद में मृतक ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई।
उठाए गये मुद्दे
मुद्दा यह उठा कि क्या यहां अभियुक्त को आपराधिक मानव वध जो हत्या कारित करता है, उसके अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है या नहीं?
निर्णय
अदालत ने वर्तमान मामले में धारा 300 (बीएनएस की धारा 101) में अपवाद 4 के अनुप्रयोग का विश्लेषण किया। यह रिकॉर्ड पर साबित हुआ कि लंबित दीवानी मुकदमा के आलोक में पक्षों के बीच अचानक मौखिक झगड़ा हुआ और यह मौखिक झगड़ा शारीरिक लड़ाई में बदल गया।
अदालत ने कहा कि धारा 300 (बीएनएस की धारा 101) के अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें विवाद की उत्पत्ति में कुछ उकसावे दिए गए हों या जो भी झगड़े का कारण था। फिर भी दोनों पक्षों के बाद के आचरण ने उन्हें अपराध के संबंध में समान स्तर पर रख दिया।
चूँकि वर्तमान मामले में झगड़ा बिना किसी सुधार के अचानक लड़ाई में बदल गया, इसलिए पूरी घटना सहज थी। इसलिए, इन परिस्थितियों के आलोक में, अभियुक्त को धारा 300 (बीएनएस की धारा 101) के अपवाद 4, के अनुप्रयोग के कारण आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, के लिए दोषी ठहराया गया है।
जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1991)
तथ्य
इस मामले में, मृतक ने अज्ञा देवी से शादी की थी और उनके साथ शाहदरा, दिल्ली में उनके घर में रहता था। अभियुक्त ने अज्ञा देवी के चचेरे भाई से शादी की थी, इसलिए रिश्तेदार के रूप में मृतक के घर जाता था। मृतक को डर था कि उसकी पत्नी और अभियुक्त के बीच अवैध संबंध हैं, और इसलिए उसने उसे अपने घर आने के लिए मना किया था। 18 अगस्त 1973 को, जब मृतक घर में नहीं था, तो अभियुक्त अज्ञा देवी से मिलने आया था। जब मृतक वापस आया, तो उसका अभियुक्त से विवाद हो गया, और अभियुक्त ने अपनी कमर से कृपाण निकाला और मृतक को सीने में छुरा घोंप दिया। इस हमले से मृतक की मौत हो गई।
उठाए गये मुद्दे
अदालत के सामने मुद्दा यह था कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया था?
निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, चूंकि दोनों के बीच केवल विवाद था और कोई लड़ाई नहीं थी, धारा 300 (बीएनएस की धारा 101) में अपवाद 4 का अनुप्रयोग प्रश्न से बाहर था।
दूसरे, अदालत ने आईपीसी की धारा 300 तीसरे (बीएनएस की धारा 101(c)) की सामग्री की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त कृपाण लेकर मृतक के घर गया, और बीमार की छाती पर वार किया, जो शरीर का वह एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, जो मृतक की मृत्यु का कारण बना।
अदालत ने इस तथ्य की भी जांच की कि अभियुक्त द्वारा केवल एक ही झटका दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह वार की संख्या नहीं बल्कि इस्तेमाल किए गए हथियार और हमले के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि क्या सामान्य परिस्थितियों में, चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि अभियुक्त ने जानबूझकर किसी घातक हथियार से वह चोट पहुँचाई, इसलिए, उसे हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।
मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, आदि (1983)
तथ्य
इस मामले में दो परिवारों के बीच दुश्मनी के कारण पांच गांवों में तेजी से हुई पांच घटनाओं की एक श्रृंखला में 17 लोगों की जान चली गई। 12 अगस्त और 13 अगस्त 1977 की रात को अमर सिंह से संबंधित 17 लोगों की जान चली गई। इन घटनाओं के कारण मच्छी सिंह और उसके 11 साथियों पर पांच मामलों में मुकदमा चलाया गया। मच्छी सिंह को दो अन्य लोगों के साथ मौत की सजा सुनाई गई।
उठाए गये मुद्दे
अदालत के सामने मुद्दा यह था कि क्या अपराध में कुछ असामान्य या अत्यंत घृणित था, जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है?
निर्णय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, केवल अत्यंत गंभीर दोषी मामलों में ही मृत्युदंड का आदेश दिया जाना चाहिए। इस विशेष मामले में, परिस्थितियाँ बताती हैं कि यह वास्तव में पीड़ितों की निर्मम हत्या थी, जो असहाय और असुरक्षित थे। पीड़ितों से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे अमर सिंह के परिवार से थे। हत्या का तरीका बेहद नृशंसता और क्रूरता का था, अभियुक्तों ने नाबालिग बच्चों, असहाय महिलाओं और एक वयोवृद्ध (वेट्रन) दम्पति सहित अन्य लोगों की भी हत्या कर दी। इसके अलावा, पीड़ित अभियुक्त का कोई प्रतिरोध नहीं कर सके। अत: इन परिस्थितियों में आजीवन कारावास से भी कड़ी सजा की आवश्यकता है।
बीएनएस, 2023 की धारा 101 (आईपीसी, 1860 की धारा 300) के अपवाद
बीएनएस 2023 का अध्याय III सामान्य सुरक्षा प्रदान करता है। ये वे बचाव हैं जिन्हें यदि अभियुक्त सफलतापूर्वक साबित कर देता है, तो वह सभी आरोपों से बरी होने के योग्य हो जाएगा। ये बीएनएस, 2023 में प्रदान किए गए सभी अपराधों पर समान रूप से लागू होते हैं। हालांकि, धारा 101 के तहत ही, कुछ विशिष्ट असाधारण परिस्थितियाँ प्रदान की गई हैं, जो यदि अभियुक्त द्वारा स्थापित की जाती हैं, तो उसका अपराध हत्या से कम होकर आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी में नहीं आते है, में बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या (1976) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 101 की चार शर्तों में से एक का अस्तित्व आपराधिक मानव वध को हत्या में बदल देगा, जबकि विशेष अपवादों से हत्या के अपराध को आपराधिक मानव वध जो हत्या के श्रेणी में नहीं आते है, उनमे बदल देंगे।
प्रासंगिक मामलो के साथ इन अपवादों पर नीचे चर्चा की गई है।
अपवाद 1
धारा 101 के अपवाद एक के अनुसार, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं तो हत्या का अपराध आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते हैnमे बदल जाएगा:
- यदि अपराधी को आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित कर दिया गया
- आत्म-नियंत्रण की हानि एक गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी
- आत्म-नियंत्रण से वंचित रहते हुए, वह किसी अन्य व्यक्ति को उकसाने या गलती या दुर्घटना से मृत्यु का कारण बनता है
- हालांकि, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए
- हत्या के बहाने के रूप में अपराधी द्वारा स्वेच्छा से उकसाया गया
- उकसावे की कार्रवाई कानून का पालन करते हुए या किसी लोक सेवक द्वारा अपनी वैध शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए कार्य के कारण नहीं होनी चाहिए
- निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के वैध प्रयोग में किये गये कार्य द्वारा
वास्तव में, यह एक प्रश्न है कि क्या कोई विशेष उकसावा इतना गंभीर और अचानक था कि उसे अपवाद के अंतर्गत शामिल किया जा सके।
आर बनाम डफी (1949), के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति गोडार्ड, ने उकसावे को परिभाषित किया है “उकसावा कुछ कार्य या कार्यों की एक श्रृंखला है जो मृत व्यक्ति द्वारा अभियुक्त के प्रति की जाती है जो किसी भी उचित व्यक्ति को और वास्तव में अभियुक्त को, आत्म-नियंत्रण का अचानक और अस्थायी नुकसान पहुचाएगा, जो अभियुक्त को इस तरह से भावना के अधीन कर देगा कि वह क्षण भर के लिए स्व विवेक से बाहर हो जाएगा”।
के.एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961)
तथ्य: इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अभियुक्त एक नौसेना अधिकारी था, जिस पर अपनी पत्नी के प्रेमी आहूजा की हत्या के लिए आईपीसी, 1860 की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया था। घटना वाले दिन अभियुक्त की पत्नी ने उसके सामने आहूजा के साथ अपने नाजायज रिश्ते की बात कबूल की थी। उसी दिन, वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक फिल्म देखने ले गया, और वह अपने जहाज पर गया, रिवॉल्वर ली और आहूजा के घर चला गया। उनके बीच विवाद और संघर्ष हुआ, इस दौरान दो गोलियां चलाई गईं, जो आहूजा को लगीं।
उठाए गये मुद्दे: क्या वर्तमान मामले में अभियुक्त को अपवाद का लाभ दिया जा सकता है?
निर्णय: बचाव पक्ष द्वारा अपवाद का दावा किया गया कि अचानक गंभीर उकसावे के कारण अभियुक्त आत्म-नियंत्रण की शक्ति से बाहर हो गया और उसने मृतक को गोली मार दिया। प्रश्न यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आहूजा ने अपवाद के तहत नानावती को उकसाया था? और इसके अलावा, क्या उकसावे की कार्रवाई गंभीर और अचानक थी?
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या अभियुक्त के समान पद पर बैठा एक उचित व्यक्ति अपनी पत्नी द्वारा व्यभिचार (एडल्ट्री) की स्वीकारोक्ति पर उसी तरह से प्रतिक्रिया करता जिस तरह से अभियुक्त ने प्रतिक्रिया की थी।
इस प्रश्न का उत्तर देने में विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, सबसे पहले इस बात पर विचार करना कि क्या उकसावे के बाद एक उचित व्यक्ति को शांत होने का समय देने के लिए पर्याप्त अंतराल समाप्त हो गया है और दूसरी बात, उस उपकरण को ध्यान में रखना होगा जिसके साथ मानव वध प्रभावित हुआ था। आवेग की गर्मी में एक साधारण वार, छिपाकर किए गये खंजर जैसे घातक हथियार का उपयोग करने से बहुत अलग है, इसलिए यदि अपवाद का दावा किया जाना है तो चोट का तरीका उकसावे के लिए उचित होना चाहिए।
अदालत ने जांच के लिए प्रासंगिक भारतीय कानून के अनुप्रयोग के अपवाद की जांच के लिए आगे कहा कि:
- गंभीर और अचानक उकसावे का परीक्षण यह है कि क्या समाज के उसी वर्ग से संबंधित एक उचित व्यक्ति, जिस स्थिति में अभियुक्त को रखा गया था, उसे इतना उकसाया जाएगा कि वह अपना आत्म-नियंत्रण खो देगा।
- शब्द और इशारे भी कुछ परिस्थितियों में, उसके कार्य को इस अपवाद के अंतर्गत लाने के लिए गंभीर और अचानक उकसावे का कारण बन सकते हैं
- पीड़ित के पिछले कार्य से बनी मानसिक पृष्ठभूमि को यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है कि क्या बाद के कार्य अपराध करने के लिए गंभीर और अचानक उकसावे का कारण बना।
- घातक वार स्पष्ट रूप से उस उकसावे से उत्पन्न जुनून के प्रभाव के कारण होना चाहिए, न कि समय बीतने या अन्यथा से जुनून ठंडा होने के बाद, पूर्व-चिंतन और गणना के लिए जगह देना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने होम्स बनाम लोक अभियोजन के निदेशक (1946) मामले का हवाला दिया। जहां न्यायमूर्ति साइमन ने कहा कि “उकसावे से संबंधित संपूर्ण सिद्धांत इस तथ्य पर निर्भर करता है कि यह आत्म-नियंत्रण के अचानक और अस्थायी तरह से खोने का कारण बनता है या पैदा कर सकता है, जिससे द्वेष, जो किसी को मारने या शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने के इरादे का गठन होता है, और नकारात्मक हो जाता है।

अदालत ने अंततः माना कि जब अभियुक्त की पत्नी ने उसके सामने अपने व्यभिचारी व्यवहार के बारे में कबूल किया, तो हम आत्म-नियंत्रण की क्षणिक हानि मान सकते हैं। हालांकि, अपनी पत्नी और बच्चों के भविष्य के बारे में आहूजा से स्पष्टीकरण मांगने का उनका आचरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन्होंने अपना आत्म-नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके अलावा, उन्होंने पूरे दिन की योजना बनाई थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों को सिनेमा देखने ले गया, अपने जहाज पर गया, छह गोलियों से भरी एक रिवॉल्वर ली और अपनी कार चलाकर पहले कार्यालय गया, और फिर बाद में आहूजा के फ्लैट पर गया। वह दोपहर 1:30 बजे अपने घर से निकला और शाम 4:20 बजे हत्या हो गई। उसके पास अपना आत्म-नियंत्रण हासिल करने के लिए पर्याप्त समय था, केवल तथ्य यह है कि गोली मारने से पहले, मृतक ने अभियुक्त को गाली दी थी और गाली ने उसे उकसाया था। अपमानजनक उत्तर हत्या के लिए उकसाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए, अदालत ने आईपीसी, 1860 की धारा 100 के अपवाद एक का लाभ देने से इनकार कर दिया और अभियुक्त को बीएनएस, 2023 की धारा 101 के तहत दोषी ठहराया।
अपवाद 2
धारा 101 के अपवाद 2 के अनुसार, हत्या का कार्य आपराधिक मानव वध o हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा में बदल जाएगा, यदि:
- अपराधी निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग सद्भावना के साथ कर रहा था
- उन्होंने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया
- वह एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना जिसके विरुद्ध वह अपने बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहा था
- ऐसी मृत्यु बिना निवारण के और आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाने के इरादे के बिना की जानी चाहिए।
जहां अभियुक्त ने दूसरे की हत्या कर दी, जबकि वह बीएनएस, 2023 के तहत प्रदान किए गए धारा 34-44 (आईपीसी की धारा 96–106) के तहत सद्भावना में अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहा था। हालांकि, उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और मृत्यु का कारण बना। मृत्यु किसी पूर्व-चिंतन से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उसे बचाव के लिए आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से कार्य नहीं करना चाहिए।
कट्टा सुरेंद्र बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008), के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘निजी बचाव के अधिकार का अधिकार बढ़ाने’ और ‘निजी बचाव का अधिकार समाप्त हो जाने के बाद कार्य करने’ की स्थिति के बीच अंतर किया। बाद के मामले में, अपवाद लागू नहीं होगा क्योंकि अभियुक्त को अब निजी बचाव का अधिकार नहीं था और इस तरह वह इसका उल्लंघन नहीं कर सकता था।
नाथन बनाम मद्रास राज्य (1972), के मामले में अभियुक्त का कुछ जमीन पर कब्जा था जो उसने मृतक से पट्टे (लीज) पर ली थी। कुछ लगान बकाया हो गया था जिसके कारण मृतक जमींदार ने जबरदस्ती अभियुक्त को बेदखल कर उसकी फसल काटने की कोशिश की। अपनी संपत्ति के खिलाफ निजी बचाव की प्रयोग में, अभियुक्त ने मृतक पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अदालत ने कहा कि अभियुक्त के पास अपनी निजी बचाव का प्रयोग करने का कानूनी अधिकार है। हालांकि, मृतक जमीनदार कोई घातक हथियार नहीं लिए था, इसलिए अभियुक्त की ओर से मौत या गंभीर चोट का कोई डर नहीं था। इसलिए, उनकी निजी बचाव आईपीसी की धारा 104 (बीएनएस, 2023 की धारा 42) के तहत मौत के अलावा किसी भी नुकसान पहुंचाने की सीमा तक सीमित थी। चूँकि उसने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया था, इसलिए धारा 300 का अपवाद 2 लागू हुआ, और उसका अपराध आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं कारित करता है, मे बदल दिया गया था।
अपवाद 3
धारा 101 के अपवाद 3 के अनुसार, हत्या का अपराध आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं कारित करता है, मे बदल जाएगा यदि:
- अपराधी एक लोक सेवक था या सार्वजनिक न्याय को आगे बढ़ाने में लोक सेवक की सहायता करने वाला व्यक्ति था।
- उसने कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति को पार कर लिया
- वह सद्भावना से काम करते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बना
- वह कार्य व्यक्ति के प्रति बिना किसी दुर्भावना के होना चाहिए और एक लोक सेवक के रूप में उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए वैध और आवश्यक होना चाहिए।
दाखी सिंह बनाम राज्य (1955) के मामले में पुलिस अधिकारी ने एक चोर को गिरफ्तार किया था और उसे ट्रेन में ले जा रहा था। हालांकि, चोर चलती ट्रेन से भाग गया और पुलिस अधिकारी ने उसका पीछा करने की कोशिश की। जब पुलिस अधिकारी उसे पकड़ने की स्थिति में नहीं था, तो उसने उस पर बंदूक से गोली चला दी, लेकिन अनजाने में वह गोली फायरमैन को लग गई और उसकी मौत हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये मामला अपवाद 3 के अंतर्गत आएगा।
अपवाद 4
धारा 101 के अपवाद 4 के अनुसार, हत्या का अपराध आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं करता है, उसमे बदल जाएगा, जहां:
- जोश में आकर अचानक हुई मारपीट से मौत हो जाती है
- लड़ाई अचानक झगड़े में बदल जाए।
- अभियुक्त को बिना किसी पूर्व चिंतन के, बिना अनुचित लाभ उठाए और बिना क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य करना चाहिए।
यह जांचना महत्वहीन है कि क्या यह अभियुक्त था या पीड़ित, जिसने पहले उकसावे या हमले की पेशकश की थी। ऐसी परिस्थिति में लड़ाई का अस्तित्व एक शर्त है, परन्तु जहां कोई लड़ाई ही नहीं है, वहा अपवाद आकर्षित नहीं होता है जैसा कि जसवन्त सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1998) के मामले में कहा गया है।
शब्द ‘लड़ाई’ मौखिक झगड़े से अधिक कुछ दर्शाती है, जैसा कि केसर सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2008) में कहा गया है, जो की झड़प के आदान-प्रदान की मांग करता है।
मोहम्मद मिथेन शाहुल हामिद बनाम केरल राज्य (1980) में कहा गया है कि एक लड़ाई में दोनों पक्षों द्वारा हमला किया जाना चाहिए ना कि एक पक्ष द्वारा हमला और दूसरे द्वारा पीछे हटना लड़ाई नहीं है।
धर्मन बनाम पंजाब राज्य (1956) के मामले में अभियुक्त और मृतक के बीच जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद था। मृतक ने विवादित जमीन पर चूना तोड़ने की मशीन लगायी थी, जिसे अभियुक्त ने तोड़ दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और परिणामस्वरूप मृतक पर जानलेवा वार हुए। अदालत ने माना कि अचानक बिना किसी बचाव के लड़ाई हुई और अचानक जुनून मे हुए झगड़े के वजह से चोटें आई थीं। इसके अलावा, अभियुक्त की ओर से कोई अनुचित लाभ या क्रूर कार्य नहीं किया गया। इसलिए, अपवाद 4 वर्तमान मामले पर लागू होगा।
अपवाद 5
धारा 101 के अपवाद 5 के अनुसार, हत्या के अपराध को आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, मे बदल दिया जाएगा, जहां पीड़ित बालिग है और उसने मृत्यु या मृत्यु का जोखिम सहने की सहमति दी है। दशरथ पवन बनाम बिहार राज्य (1957) के मामले में, अभियुक्त दसवीं कक्षा का छात्र था जो अपनी परीक्षा में तीन बार फेल हो चुका था। अपनी असफलताओं से निराश होकर उसने अपनी जान लेने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने पहले उसे मारने और फिर खुद को मारने के लिए कहा। समझौते के अनुसार, अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी जान ले पाता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपवाद 5 का लाभ दिया गया।
बीएनएस, 2023 की धारा 101 के अपवादों पर मामले
किशोर सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977)
तथ्य
इस मामले में अपीलकर्ता ने 28 जुलाई, 1968 को मृतक जवाहर और पूरन सिंह पर हमला किया और ‘सब्बल’ और कुल्हाड़ी के कुंद सिरे का उपयोग करके मृतक को गंभीर चोटें पहुंचाई। सिर की चोटों के लिए सर्जिकल ऑपरेशन से उबरने के बाद जवाहर की मृत्यु 27 अगस्त, 1968 को अस्पताल में हो गई ।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त को पीड़िता की हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है?
निर्णय
इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विश्लेषण करने के बाद कहा। यह स्पष्ट है कि वहाँ “तीन डॉक्टरों द्वारा मौत के कारण के संबंध में दिए गये राय कुछ हद तक संकोचपूर्ण चिकित्सकीय राय है ” इसके अलावा, मृतक की मृत्यु घटना के एक महीने बाद हुई। इसलिए, धारा 300 तीसरी इन तथ्यों पर स्थापित नहीं हुई थी, चूंकि धारा 300 साबित नहीं हुई, इसलिए अभियुक्त द्वारा अपवादों को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता है। अभियोजन पक्ष यह कहकर तत्वों को साबित करने के अपने बोझ को हल्का नहीं कर सकता है कि अभियुक्त ने अपवादों के अनुप्रयोग की पैरवी नहीं की है या उसे साबित नहीं किया है।
अदालत ने आगे बताया कि धारा 300 के अपवादों को लागू करने के साथ, धारा 300 के सभी आवश्यक तत्वों को स्थापित करने का बोझ सबसे पहले अभियोजन पक्ष पर पड़ता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि हत्या का अपराध साबित हो जाता है, तो धारा 300 के तहत किसी भी अपवाद को लागू करने से अपराध को आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, उनमे बदल दिया जाएगा। हालांकि ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ने किसी भी अपवाद की प्रयोज्यता का अनुरोध नहीं किया है, धारा 300 (बीएनएस की धारा 101) के तहत हत्या के अपराध की आवश्यक सामग्री को साबित करने का प्रारंभिक दायित्व अभी भी अभियोजन पक्ष पर है। आगे न्यायालय ने कहा कि, “यदि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 300 के चार खंडों में से किसी एक को स्थापित करने में इस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो हत्या का आरोप नहीं बनाया जाएगा और मामला आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, उसका हो सकता है क्योंकि यह आईपीसी की धारा 299 के तहत वर्णित है।”
बीएनएस, 2023 की धारा 103 तहत हत्या के लिए सजा
हत्या के अपराध के लिए सज़ा के दो विकल्प दिए गए हैं। पहला मौत और दूसरा आजीवन कारावास। इन सजाओं के अलावा अभियुक्त को जुर्माना भी भरना होगा।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 में हत्या की सजा के लिए एक नई उपधारा जोड़ी गई है।
धारा 103(2): “जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा।”
वास्तव में, नई जोड़ी गई उपधारा, लोगों के एक गैरकानूनी समूह को सामूहिक रूप से हत्या का अपराध करने से हतोत्साहित करने का प्रयास करती है। यह इस तथ्य की स्वीकृति है कि किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अपराध करने की तुलना में अन्य लोगों द्वारा समर्थित होने पर अपराध करने की अधिक संभावना होगी। इसके अलावा, नस्ल, जाति, सामुदायिक लिंग, जन्म स्थान, भाषा और व्यक्तिगत विश्वास जैसे कारक महत्वपूर्ण पहचान चिह्नक के रूप में कार्य करते हैं जो लोगों को एक साथ समूहित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए, इस धारा के तहत 5 या अधिक लोग एक साथ मिलकर ऊपर बताए गए आधार पर हत्या का अपराध करते हैं, तो समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए मौत की कठोरतम सजा या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास निर्धारित की गई है। यह दायित्व प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत योगदान की परवाह किए बिना तय किया जाएगा।

इसे संहिता की धारा 3(5) के तहत पाए जाने वाले साझा इरादे के सिद्धांतों की एक शाखा के रूप में देखा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि जब एक आपराधिक कार्य कई लोगों द्वारा ‘सभी के साझा इरादे को आगे बढ़ाने’ में किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी ऐसी होती है जैसे उसने अकेले ही कार्य किया हो। दायित्व प्रत्येक के विशेष योगदान के बावजूद है, बशर्ते कि प्रत्येक का एक ही साझा इरादा हो और उसने उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किया हो।
बीएनएस 2023 की धारा 103 के तहत मौत की सजा
भारतीय न्यायशास्त्र में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को बढ़ती महत्ता मिल रही है, जिससे कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड को सजा के रूप में देने की संवैधानिकता पर सवाल उठने लगे हैं।
एक प्रतिधारणवादी (रीटेंसनिस्ट) और उन्मूलनवादी (ऐबोलिशनिस्ट) बहस उभरी है, जहां प्रतिधारणवादी का तर्क है कि कुछ जघन्य अपराधों के लिए, मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए। जबकि उन्मूलनवादी का तर्क है कि मानवाधिकारों की प्रधानता के युग में मृत्युदंड का कोई स्थान नहीं है। स्थिति पेनोलॉजी के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्रतिधारणवादी निवारण और प्रतिशोध के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, जबकि उन्मूलनवादी पुनर्वास और सुधार के सिद्धांत में विश्वास करते हैं।
भारत में, 1860 की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और 2023 की भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) दोनों कुछ बहुत ही जघन्य अपराधों के लिए सजा के रूप में मौत की सजा का प्रावधान रखती हैं, उनमें से एक हत्या है। प्रत्येक मामले में मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा देने के निर्णय के प्रश्न पर बीएनएसएस की धारा 393(3) (सीआरपीसी 1973 के धारा 354(3)) पर विचार करना होगा। यह धारा अदालत को विशेष सजा देने के लिए कारण रिकॉर्ड करने का कर्तव्य देती है और इसके अलावा, मृत्युदंड दिए जाने की स्थिति में विशेष कारण दर्ज करने होते हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा शुरू की गई एक परियोजना, प्रोजेक्ट 39-A, द्वारा प्रकाशित “ विचारण न्यायालय में सुनाई गई मृत्युदंड की सजा” शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने सत्र न्यायालय द्वारा आयोजित मृत्युदंड की सजा सुनाने वाली सुनवाई की सतही प्रकृति का पर्दाफाश किया है और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के फैसले द्वारा भारत में निर्धारित मृत्युदंड ढांचे में आदर्श और प्रक्रियात्मक अंतरालों को प्रदर्शित किया है।
वर्ष 1980 तक, एक प्रकार की शून्यता थी कि कौन से मामले मृत्युदंड के दायरे में आएंगे और कौन से नहीं, लेकिन अब असाधारण और दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत ने इसके लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में विकसित किया गया था। यह कहा गया कि अदालत को अपना विचार मुख्य रूप से अपराध तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपराधी की परिस्थितियों पर भी उचित विचार करना चाहिए। ऐसा तभी होता है जब दोषी अत्यधिक भ्रष्टता के अनुपात को मान लेता है कि विशेष कारणों को वैध रूप से अस्तित्व में माना जा सकता है। न्यायधीशों को खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। मामले से अनुमान लगाए जा सकने वाले कुछ दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:
- अत्यधिक गंभीर मामलों में दोषी होने को छोड़कर, मौत की अत्यधिक सज़ा नहीं दी जा सकती
- मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले, अपराध की परिस्थितियों के साथ-साथ अपराधी की परिस्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है
- आजीवन कारावास नियम है, जबकि मृत्युदंड एक अपवाद है और केवल तभी दिया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास अपराध और अपराधी की परिस्थितियों के संबंध में अपर्याप्त लगता है।
- बढ़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए।
इसके अलावा, अदालत को दो प्रश्न भी बनाने चाहिए जिनका उत्तर सजा तय करते समय दिया जाना चाहिए
- क्या उस अपराध में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा की मांग करता है?
- क्या अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि परिस्थितियों को कम करने के लिए अधिकतम महत्व दिए जाने के बाद भी उस सज़ा को लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?
मच्छी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न स्थितियों को निर्धारित किया है, जो दुर्लभतम मामलों के अंतर्गत आएंगे। ये इस प्रकार हैं:
- जब की गई हत्या अत्यंत क्रूर, हास्यास्पद, शैतानी, विद्रोही या निंदनीय होती है, तो इससे समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश जागृत होता है। उदाहरण के लिए, किसी को जिंदा जलाने के इरादे से उसके घर में आग लगाना;
- अपराध की भयावहता बड़े पैमाने पर है, जिसका अर्थ है कई लोगों की मौत होना; या जहां बड़े पैमाने पर नरसंहार (मैसकर), एक समुदाय के लोगों की हत्या आदि होती है;
- जब मृत्यु व्यक्ति की जाति और धर्म के कारण होती है;
- जब अभियुक्त के इरादे क्रूर थे या पूर्ण भ्रष्टता का संकेत देते थे; और
- जब हत्या का शिकार एक मासूम बच्चा, एक असहाय महिला या व्यक्ति (बुढ़ापे या दुर्बलता के कारण), एक सार्वजनिक व्यक्ति, आदि है और क्रूर तरीके से किया जाता है।
- एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जिसने हत्यारों पर बहुत भरोसा किया।
कानूनी प्रस्ताव के रूप में, इस बात पर सहमति पर पहुंचना मुश्किल होगा कि मृत्युदंड कहाँ दिया जाना चाहिए और कहाँ नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लेने का मामला है और कोई सीधा सूत्र नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि कोई भी दो अपराध समान नहीं होते हैं। यह अभी भी निर्धारित करने के लिए व्यक्तिपरक है कि सबसे दुर्लभ में क्या है और क्या नहीं है। इसलिए यह एक अस्पष्टता छोड़ देता है कि किन मामलों में मृत्युदंड लागू किया जा सकता है।
अपराध के अभियुक्तों को मौत की सज़ा दिए जाने का सबसे ताज़ा मुकेश और अन्य बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य (2017) (निर्भया मामला), मामला है। जहां एक किशोर को छोड़कर सभी अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई गई और आखिरकार 2020 में सजा पर अमल किया गया। इस फांसी ने मौत की सजा के मुद्दे को देश भर में कई गरमागरम बहसों का केंद्र बना दिया। प्रमुख प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या अन्य देशों की तरह भारत को भी मृत्युदंड समाप्त कर देना चाहिए, जबकि न्यायपालिका के पास आजीवन कारावास जैसा विकल्प मौजूद है।
निर्भया मामले में फांसी के बाद, मौत की सजा के मुद्दे पर जनता द्वारा विभिन्न दलीलें पेश की गईं। मौत की सजा को बरकरार रखने का समर्थन करने वाले समूह ने तर्क दिया कि जो लोग हत्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और की जान ले ली है, उन्होंने अपना जीवन जीने का अधिकार खो दिया है या यह कि दोषी हत्यारों को मारकर, हम संभावित हत्यारों को लोगों की हत्या करने से रोक देंगे। दूसरी ओर, अनुच्छेद 21 और मानव जीवन को बढ़ती हुई महत्ता के साथ, मौत की सजा के उन्मूलन की आवाजें पहले से कहीं ज्यादा तेज हुई हैं। उनका तर्क है कि प्रतिशोध और आँख के बदले आँख के विचार को सुधार और पुनर्वास के विचार को रास्ता देना चाहिए। इसके अलावा, वे तर्क देते हैं कि मौत की सजा के निरोधक प्रभाव को किसी भी सबूत से स्थापित नहीं किया गया है।
जिंदल व्यवहारिक विज्ञान संस्थान द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, इस अध्ययन का उद्देश्य मृत्युदंड के प्रति जनता के दृष्टिकोण, अपराध के प्रकार और परिस्थितियों का आकलन करना था, जिनके लिए मृत्युदंड का पक्ष लिया जाता है, अनुभवजन्य (एम्पिरिकल) अनुसंधान के निष्कर्षों के अनुसार, यह देखा गया है कि भारी बहुमत 79% उत्तरदाताओं का कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए मृत्युदंड को वैध बनाने का पक्षधर है।
आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, और आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी मे आते है दोनों के बीच संबंध:
| क्र.सं. | बीएनएस, 2023 की धारा 100- आपराधिक मानव वध | बीएनएस, 2023 की धारा 101- आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी मे आते है। | दोनों में अंतर |
| 1. | मृत्यु कारित करने का इरादा | मृत्यु कारित करने का इरादा | कोई अंतर नहीं- मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य सीधे तौर पर हत्या के अपराध के अंतर्गत आएगा। |
| 2. | ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। | ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिसके बारे में अपराधी जानता हो कि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है जिसे नुकसान पहुंचाया गया है। | जबकि धारा 100 में केवल शारीरिक चोट की संभावना है, धारा 101 में, विशेष पीड़ित के बारे में व्यक्तिपरक ज्ञान आवश्यक है। |
| 3. | ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। | किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा और पहुंचाई जाने वाली शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। | धारा 100 के तहत शारीरिक चोट से केवल मृत्यु होने की संभावना है; हालांकि धारा 101 के लिए शारीरिक चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए ‘पर्याप्त’ होनी चाहिए |
| 4. | यह ज्ञान कि ऐसे कार्य से मृत्यु होने की संभावना है। | यह ज्ञान कि यह कार्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि इसके कारण पूरी संभावना है, की मृत्यु होनी चाहिए, या ऐसी शारीरिक चोट लगनी चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। | धारा 100 के तहत आवश्यक ज्ञान केवल मृत्यु की संभावना के बारे में है, जबकि धारा 101 के तहत ज्ञान सभी संभावनाओं में मृत्यु के कारण के बारे में है। |
रेग बनाम गोविंदा का ऐतिहासिक मामला (1876)
रेग बनाम गोविंदा (1876) यह सबसे ऐतिहासिक मामलों में से एक है जो आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, और हत्या के बीच अंतर और संबंध से संबंधित है, जिसे रेग बनाम गोविंदा (1876) मामले में स्पष्ट किया गया था। मामले के तथ्यों के अनुसार, एक दंपत्ति के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद, उसने अपना घुटना उसकी छाती पर रख दिया और बंद मुट्ठी से उसके चेहरे पर दो या तीन जोरदार वार किए। चोटों के कारण पत्नी की कुछ ही देर बाद मौत हो गई। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, यह कहा गया कि मृत्यु मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह के कारण हुई। न्यायमूर्ति मेलविल ने मामले का फैसला करते हुए बीएनएस, 2023 की धारा 100 और बीएनएस, 2023 की धारा 101 (पहले क्रमशः धारा 299 और 300 आईपीसी, 1860) के बीच अंतर को स्पष्ट किया।
अदालत ने दोनों धाराओं के बीच के अंतर को निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया।

“धारा 299 और धारा 300 का पहला भाग बताता है कि जहां मारने का इरादा हो, वहां अपराध हमेशा हत्या होता है।
धारा 299 और धारा 300 का तीसरा भाग, चौथा भाग मुझे उन मामलों पर लागू करने के लिए प्रतीत होता है जिनमें मृत्यु या शारीरिक चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अपराध आपराधिक मानव वध है या नहीं, यह मानव जीवन को खतरे की डिग्री पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु संभावित परिणाम है, तो यह आपराधिक मानव वध है; यदि यह सबसे संभावित परिणाम है, तो यह हत्या है।
दूसरे शब्दों में, धारा 300 का सार… “अपराध हत्या है, यदि अपराधी जानता है कि विशेष व्यक्ति को संविधान की विशिष्टता, अपरिपक्व आयु या अन्य विशेष परिस्थितियों से, ऐसी चोट से मार दिया जाए, जो सामान्य रूप से मृत्यु का कारण नहीं बनेगी।”
धारा 299 के दूसरे भाग और धारा 300 के तीसरे भाग पर विचार करना बाकी है, और इन दोनों खंडों की तुलना पर ही वर्तमान जैसे संदिग्ध मामलों का निर्णय आम तौर पर निर्भर होना चाहिए। यह अपराध आपराधिक मानव वध है, यदि पहुंचाई जाने वाली शारीरिक चोट से मृत्यु होने की संभावना हो; और यदि ऐसी चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, तो यह हत्या है।”
इसलिए, वर्तमान मामले में, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त का मौत का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था, न ही मृतक के बारे में कोई अनोखी बात थी जिसके बारे में अभियुक्त को पता था और न ही जो शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था, जो सामान्य कारण मे मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, बल्कि यह केवल मृत्यु का कारण बनने की ‘संभावना’ थी। इस मामले में मृत्यु मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह के कारण हुई थी; इसलिए, अभियुक्त को आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते है, के अपराध का दोषी ठहराया गया।
इसलिए, वर्तमान मामले में, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त का मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था, न ही मृतक के बारे में कोई ऐसी ख़ासियत थी जिसके बारे में अभियुक्त जानता था और न ही शारीरिक चोट जो पहुंचाने का इरादा था, सामान्य कारणों से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, बल्कि यह केवल ‘संभावित’ थी मृत्यु का कारण। मामले में मृत्यु मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह के कारण हुई थी; इसलिए, अभियुक्त को हत्या की मात्रा तक नहीं पहुंचने वाले दोषपूर्ण मानव हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी द्वारा की गई हत्या के लिए बीएनएस, 2023 की धारा 102 (आईपीसी, 1860 की धारा 303) के तहत सजा
बीएनएस, 2023 की धारा 102, जो आईपीसी, 1860 की धारा 303 से मेल खाती है, एक विशेष मामले में हत्या के लिए सजा से संबंधित है। जहां कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और जब वह सजा प्रभावी होती है, तो हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड या वैकल्पिक रूप से आजीवन कारावास, जिसका अर्थ है उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए, से दंडित किया जाएगा।
आईपीसी, 1860 की धारा 303 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983) मामले में असंवैधानिक माना गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि यह धारा असंवैधानिक और शून्य है क्योंकि यह समानता की गारंटी जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, किसी व्यक्ति के जीवन या निजी स्वतंत्रता से वंचित करने पर रोक लगाता है, का उल्लंघन करती है। अदालत ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा के दौरान हत्या करने वाले व्यक्तियों और ऐसे व्यक्ति जो तब हत्या करने है जन ऐसी सजा के अधीन नहीं हैं के बीच सजा के मामले में अंतर करने के लिए उचित तर्कसंगत औचित्य का अभाव है।
असंवैधानिकता का तत्व इस तथ्य के कारण था कि ऐसे अपराधी के मामले में केवल मौत की सजा निर्धारित की गई थी। हालाँकि, अब बीएनएस, 2023 के तहत मृत्यु और आजीवन कारावास के बीच विकल्प प्रदान किया गया है। जिससे असंवैधानिकता के तत्व का निवारण हो गया है।

बीएनएस, 2023 की धारा 102 के तहत द्वेष के हस्तांतरण का सिद्धांत
‘जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के कारण आपराधिक मानव वध’ की धारणा बीएनएस, 2023 की धारा 102 (आईपीसी, 1860 की धारा 301) में निहित है, जिसमें कहा गया है कि:
आपराधिक मानव वध तब होता है जब कोई व्यक्ति, यह इरादा रखते हुए या यह जानते हुए कि उनके कार्यों से मृत्यु होने की संभावना है, अनजाने में उस व्यक्ति जिसे वे मारना चाहते थे या जानते थे कि मारे जाने की संभावना है, के अलावा किसी और की मृत्यु का कारण बनता है। ऐसे मामले में, आपराधिक मानव वध को उसी तरह वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि व्यक्ति अपने इच्छित या अपेक्षित शिकार की मृत्यु का कारण बना हो।
दूसरे शब्दों में, B के प्रति उसका जो भी द्वेष था वह C में स्थानांतरित हो गया। B के प्रति उनका वही इरादा या ज्ञान उसके उस कार्य में स्थानांतरित हो गया जिसने C को मार डाला।
- केवल आपराधिक मनःस्तिथि ही हस्तांतरित की जाएगी जो अभियुक्त के पास शुरू में थी।
- द्वेष के हस्तांतरण के लिए यह आवश्यक है कि उत्पन्न प्रभाव लेन-देन की निरंतरता में रहे।
- द्वेष के हस्तांतरण का यह सिद्धांत सभी अपराधों पर लागू होता है और बीएनएस की धारा 102 तक सीमित नहीं है।
इसे अंग्रेजी कानून में “स्थानांतरित द्वेष का सिद्धांत’ या ‘उद्देश्य का स्थानांतरण’ या ‘स्थानांतरित इरादा’ के रूप में भी जाना जाता है। आपराधिक मनःस्थिति आम तौर पर अपराध के सबूत का एक अनिवार्य तत्व है। इसे सजा से बचने के लिए एक दलील के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जब आकस्मिक परिस्थितियों के कारण अभियुक्त के कार्य के कारण अपराधी द्वारा अपेक्षित परिणाम नहीं आता है।
उदाहरण के लिए, A, B को मारने के इरादे से उस पर गोली चलाता है, लेकिन B बच जाता है और गोली C को मार देता है। यहां A की गोली के परिणामस्वरूप C की मृत्यु हो गई; यदि उसने B को मारने के इरादे से उसे गोली नहीं मारी होती तो वह नहीं मरता, इसलिए, कहा जाता है कि B के प्रति द्वेष C में स्थानांतरित हो गया है। हालांकि, इस सिद्धांत में केवल एक चेतावनी है, जो है ‘ कम ग्रेनो सालिस’ जिसका मतलब है कि व्यक्ति का कार्य एक ही अपराध का होना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि अगर A, B को गोली मारता है, जो एक इंसान है और B झुक जाता है, जिससे गोली C को लगती है, तो A आपराधिक मानव वध के लिए उत्तरदायी होगा।
हालाँकि, यदि A, B पर गोली चलाता है, जो एक कुत्ता है और चूक जाता है, और गोली C को मार देता है, जो एक इंसान है, तो वह उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि उसके पास आपराधिक मनःस्थिति किसी इंसान को नहीं बल्कि एक कुत्ते को मारने की थी।
कानूनी मामले
राजबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2006)
तथ्य
इस मामले में अपीलकर्ता ने दावा किया कि पड़ोसी ने उसके भाई के घर के परिसर पर कुछ ईंटें फेंक दीं। इसी बात को लेकर उसके पिता और अभियुक्तों के बीच कहा-सुनी भी हुई लेकिन स्थानीय लोगों ने किसी तरह मामले को सुलझा लिया। अगले दिन अभियुक्त अपने दो रिश्तेदारों के साथ बंदूकें लेकर आ गया। वे शिकायतकर्ता की दुकान के पास आए, जहां उसके पिता खड़े थे। वहां अभियुक्त ने अपने रिश्तेदारों को उसे मारने के लिए उकसाया और उन्होंने शिकायतकर्ता के पिता पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद वह घायल हो गए और गिर गए।
एक लड़की उस दुकान पर कुछ सामान खरीदने आई थी और उसे चोट लग गई और वह गिर गई। अस्पताल ले जाते समय दोनों घायलों की मौत हो गई। अभियुक्तों ने अपनी दलील में कहा कि लड़की की मौत दुर्घटनावश हुई और उसे मारने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह उस जगह से गुजर रही थी और परिणामस्वरूप, उसे चोटें लगीं और उसकी मृत्यु हो गई।
उठाए गये मुद्दे
क्या अभियुक्त को लड़की की हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जा सकता है?
निर्णय
अदालत ने कहा कि धारा 301 का सार यह है कि यदि हत्या किसी ऐसे कार्य के दौरान हुई है, जिसे व्यक्ति करना चाहता है या जानता है कि मृत्यु का कारण बनने की संभावना है, तो उसे ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि हत्यारे का वास्तविक इरादा वास्तव में पूरा हो गया हो। इस मामले में, अभियुक्त का कुछ नुकसान पहुंचाने का इरादा था और उसी के अनुसरण में, उसने गोलियां चलाईं। धारा 301 इस मामले पर लागू होगी। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और आईपीसी की धारा 301 (बीएनएस, 2023 की धारा 102) के तहत दोषी ठहराया गया।
लोक अभियोजक बनाम मुशुनुरू सूर्यनारायण मूर्ति (1912)
तथ्य
इस मामले में A का इरादा B को मारने का था और इसके लिए उसने उसे हलवा परोसा जिसमें जहर मिला हुआ था। B ने हलवे का बहुत कम हिस्सा खाया और बाकी सड़क पर रख दिया। कुछ बच्चों ने हलवा उठाकर खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गयी। A ने दावा किया कि उसका उन बच्चों को मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह उनकी हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं होना चाहिए।

उठाए गये मुद्दे
क्या बच्चों की मौत के लिए अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
निर्णय
अदालत ने उसे हत्या का दोषी ठहराया, क्योंकि B की मौत का उसका जो भी इरादा था वह उन बच्चों में स्थानांतरित हो गया था। इसलिए, B के संदर्भ में, उसे हत्या के प्रयास के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था और बच्चों के संदर्भ में, उसे हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।
कल्पित परिस्थितियों का सिद्धांत
इस सिद्धांत को एक उदाहरण की सहायता से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है:
A ने B के सिर पर मोटी छड़ी से वार किया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। A का प्रारंभिक द्वेष केवल B को गंभीर चोट पहुंचाने तक ही सीमित था। हालांकि, जब वह बेहोश होकर गिर गई, तो उसने उसे मृत मान लिया और केवल मौत को आत्महत्या के रूप में पेश करने के इरादे से, उसने उसके शरीर को छत के पंखे से लटका दिया।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत सिर पर डंडे के वार से नहीं, बल्कि फांसी लगाने से हुई थी।
सवाल यह उठा कि क्या इस मामले में A को B की हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा या नहीं?
कल्पित परिस्थितियों के सिद्धांत के अनुसार, A का आपराधिक दायित्व केवल उसके प्रारंभिक द्वेष के लिए होगा। चूँकि फाँसी देने का कार्य आपराधिक मनःस्थिति हत्या करने के इरादे से, नहीं किया गया था क्योंकि जब उसने उसके शव को लटकाया तो उसे लगा कि वह मर चुकी है।
हालाँकि, अगर उसने शव को केवल इस निश्चितता के साथ लटका दिया होता की उसकी मृत्यु होनी है, तो उसका दायित्व हत्या का होगा।
पलानी गौंडन बनाम अज्ञात (1919)
तथ्य
इस महत्वपूर्ण मामले में, तथ्य इस प्रकार थे: अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर लकड़ी के हिस्से के साथ हल का फाल मारा, जिससे उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। उसे मृत समझकर, उसने झूठा सबूत बनाने के लिए, उसे फांसी पर लटका दिया। पोस्टमार्टम में, मौत का कारण फांसी बताया गया।
उठाए गये मुद्दे
अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध क्या है?
निर्णय
मद्रास उच्च न्यायालय ने काल्पनिक परिस्थितियों के सिद्धांत को लागू किया, क्योंकि जब A ने अपनी पत्नी के शव को लटका दिया, तो उसने सोचा कि वह मर चुकी है। यहां दुर्भावना के हस्तांतरण का सिद्धांत लागू होगा, जिसका अर्थ है कि मूल कार्य के लिए A का प्रारंभिक इरादा या आपराधिक मनःस्थिति मूल बिंदु पर स्थानांतरित हो जाएगा जो वास्तव में मृत्यु का कारण बनता है। यहां जब उसने अपनी पत्नी को हल के फाल के लकड़ी के हिस्से से मारा, न कि धातु के हिस्से से, उसका इरादा केवल हमला करना था और झूठा सबूत बनाने का प्रयास करना था, इसलिए, वह केवल उन अपराधों के लिए उत्तरदायी होगा।

निष्कर्ष
हत्या और आपराधिक मानव वध के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि हत्या आपराधिक मानव वध के अधिक गंभीर रूप का प्रतिनिधित्व करती है। हत्या में, इस बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है कि क्या कार्य के परिणामस्वरूप मृत्यु होगी, जबकि आपराधिक मानव वध में कुछ अनिश्चितता शामिल होती है। बीएनएस, 2023 की धारा 100 (आईपीसी की धारा 299) के अनुसार, आपराधिक मानव वध तब होता है जब कोई कार्य मौत का कारण बनने के इरादे से किया जाता है या शारीरिक चोट जिससे मौत होने की संभावना हो पहुंचाने के इरादे से किया जाता है, या यह जानते हुए कि कार्य से मौत होने की संभावना है। इस धारा में “संभावना” शब्द का बार-बार उपयोग इस बारे में अनिश्चितता के तत्व को इंगित करता है कि क्या कार्य निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बनेगा। इसके विपरीत, हत्या को बीएनएस, 2023 (धारा 300 आईपीसी, 1860) की धारा 101 के तहत परिभाषित किया गया है।
यहाँ, “संभावना” के स्थान पर “पर्याप्त” शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अस्पष्टता को दूर करता है। इससे पता चलता है कि अभियुक्त की हरकतों से मौत निश्चित है। संक्षेप में कहें तो, जबकि आपराधिक मानव वध और हत्या दोनों में मौत का कारण शामिल है, अंतर इरादे और निश्चितता की डिग्री में निहित है। हत्या, मौत का कारण बनने के स्पष्ट इरादे के साथ अधिक गंभीर अपराध का प्रतिनिधित्व करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
शादियों और अन्य उत्सवों में जश्न में चलाने वाली गोली से होने वाली मौतों से संबंधित कानून क्या है?
भगवान सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य (2020), के मामले में सर्वोच्च न्यायालय उन लोगों के दायित्व से निपटा जो जश्न में गोलियां चलाकर दूसरों को घायल करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस मामले में सवाल यह था कि क्या अपीलकर्ता का कार्य बीएनएस, 2023 की धारा 101 या धारा 100 के तहत आएगा। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार थे: अभियुक्त के बेटे की गांव में शादी हो रही थी, और जैसे ही बारात गंतव्य पर पहुंची, उसने जश्न में गोलियां चलाईं। ये गोलियाँ पाँच लोगों को लगीं और उनमें से दो की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।
अदालत ने कहा कि हालांकि हम अभियुक्त की ओर से मौत या शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा नहीं पा सके, जिससे मौत होने की संभावना हो, उसने कोई उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए और इसलिए उससे यह जानने की उम्मीद की गई कि पास खड़े लोगो को बंदूक की गोली से चोट लग सकती है। सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल जश्न के आयोजनों में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत घातक हो सकती है। इसलिए, अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को धारा 100 और बीएनएस 2023 के धारा 105 के तहत आपराधिक मानव वध के लिए दंडनीय माना गया है।
‘पीड़ित महिला सिंड्रोम’ क्या है?
‘पीड़ित महिला सिंड्रोम‘ डॉ. लेनोरे वॉकर द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि क्यों पीड़ित महिलाएं जो अपने साथियों को मारने के लिए मजबूर होती हैं, पर वे एक जगह रिश्ते में बनी रहती हैं। भारतीय संदर्भ में इसे ‘नल्लाथंगल सिंड्रोम’ के रूप में किया गया है। हालांकि, भारत में पीड़ित महिला सिंड्रोम की कानूनी मान्यता अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। प्रतिशोध लेने वाली पीड़ित महिलाओं पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।
रेजिना बनाम किरणजीत अहलूवालिया (1992) के मामले में, इंग्लैंड और वेल्स की अदालत ने स्वीकार किया कि निरंतर दुर्व्यवहार के संचयी प्रभाव किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया और उसके कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और आगे ‘उकसावे’ की पारंपरिक समझ के रूप में एक रक्षा बहुत संकीर्ण है और लंबे समय तक घरेलू शोषण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखता है।
भारत में, श्रीमती मंजू लाकड़ा बनाम असम राज्य (2013) का मामला, गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किया गया पहला मामला है जिसमें एक पीड़ित महिला ने अपने साथी की हत्या करने के मामले में उकसावे का इस्तेमाल बचाव के रूप में किया है।
भारतीय न्याय संहिता में अन्य कौन से अपराध पाए गए हैं जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन वह संहिता की धारा 100 या धारा 101 के अंतर्गत नहीं आते है?
बीएनएस, 2023 की धारा 106 (आईपीसी, 1860 की धारा 304A), जो लापरवाही से मौत का कारण बनने के अपराध से संबंधित है, यह धारा प्रदान करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी लापरवाही से कार्य करके किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो बीएनएस, 2023 की धारा 100 के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसे 5 साल तक की अवधि की कारावास और जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा।
यह किसी व्यक्ति की मृत्यु की ओर ले जाने वाली चिकित्सा लापरवाही से भी संबंधित है, जहां 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
संदर्भ