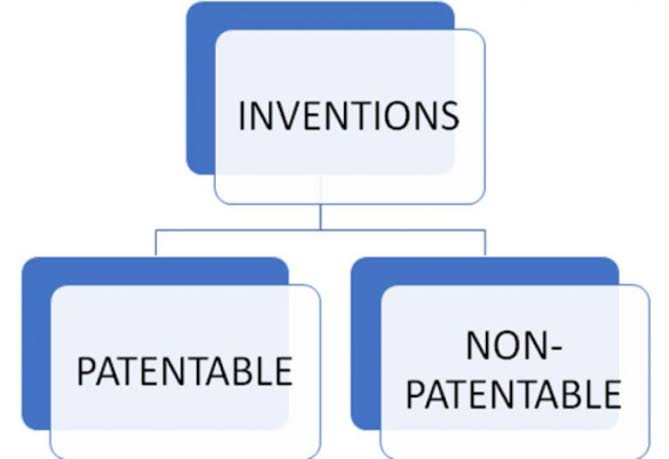यह लेख Monika Verma द्वारा लिखा गया था और आगे Jaanvi Jolly द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया था। यह लेख पेटेंट कानून के संदर्भ में ‘आविष्कार’ की अवधारणा को समझाता है, जिसमें इसकी परिभाषा और प्रासंगिक मामलो के साथ पेटेंट करने के लिए योग्यता के लिए मानदंड शामिल हैं। इसमें यह भी शामिल है कि गैर पेटेंट योग्य विषय वस्तु क्या है और यह विषय वस्तु पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। यह आगे दवा उद्योग में पेटेंट और ए.आई. की पेटेंट करने के लिए योग्यता के संबंध में स्थिति की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
पेटेंट कानून बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) कानूनों के क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र है। बौद्धिक संपदा मानव मन और रचनात्मक बुद्धि से उत्पन्न होती है। इसलिए, जो व्यक्ति अपने रचनात्मक कौशल का उपयोग करते हैं, उन्हें अपने आविष्कार के संरक्षण के रूप में लाभ का कुछ रूप दिया जाना चाहिए। यह संरक्षण पेटेंट के रूप में दिया जा सकता है। एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है।
जब पेटेंट की बात आती है, तो सभी आविष्कार सुरक्षा के लिए योग्य नहीं होते हैं। यह समझना कि किस आविष्कार को पेटेंट कराया जा सकता है और किसे नहीं, आविष्कारकों और व्यवसायों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
पेटेंट योग्य आविष्कार वे हैं जो पेटेंट कानूनों द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। आम तौर पर, एक आविष्कार पेटेंट योग्य होने के लिए, यह नहीं, गैर-स्पष्ट और उपयोगी होना चाहिए। उदाहरणों में पदार्थ के नए उपकरण, विधियां या रचनाएं शामिल हैं जो एक स्पष्ट आविष्कारशील कदम प्रदर्शित करती हैं और एक ठोस लाभ प्रदान करती हैं।
दूसरी ओर, गैर पेटेंट योग्य आविष्कार, पेटेंट संरक्षण के दायरे से बाहर हैं। इनमें अक्सर अमूर्त विचार, प्राकृतिक घटनाएं और प्रकृति के नियम शामिल होते हैं। जिन आविष्कारों में नवीनता की कमी मानी जाती है या जिन्हें मौजूदा ज्ञान के प्रकाश में स्पष्ट माना जाता है, वे भी पेटेंट योग्य नहीं हैं।
पेटेंट प्रणाली को प्रभावी ढंग से समझने और यह सुनिश्चित करने के लिए इन भेदों को समझना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा ठीक से संरक्षित है। पेटेंट के लिए योग्यता के ये आधार अलग-अलग देशों में अलग-अलग हो सकते हैं क्योंकि ये क्षेत्रीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं, इस पहलू पर अगले खंड में चर्चा की गई है।

पेटेंट कानूनों कि क्षेत्रीय प्रयोज्यता (टेरिटोरियल एप्लिकेबिल्टी)
जब हम पेटेंट कानूनों के बारे में बात करते हैं, तो वे क्षेत्रीय होते हैं, अर्थात वे उस देश के विशिष्ट कानूनों द्वारा शासित होते हैं जहां वे पंजीकृत होते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित होते हैं, हालांकि, जो देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के सदस्य हैं, उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स) के अनुरूप अपने राष्ट्रीय कानूनों को तैयार करने की आवश्यकता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की देखरेख और सुविधा प्रदान करता है और सदस्य देशों के बीच विवादों को हल करता है। ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा (आई.पी.) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए व्यापक मानक स्थापित करना है।
ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 7 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।
- यह तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है।
- यह प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजिकल) ज्ञान के उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं के पारस्परिक लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित और प्रसारित करना चाहता है। यह स्थांतरण इस तरह से होने का इरादा है जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के पक्ष में है और इसमें शामिल पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को संतुलित करता है।
ट्रिप्स समझौते द्वारा स्थापित एक व्यापक पेटेंट ढांचे के निर्माण के बावजूद, हम पेटेंट के लिए योग्यता और गैर पेटेंट के लिए योग्यता के आधार पर कुछ देश विशिष्ट भेद पा सकते हैं।
इस लेख में पेटेंट योग्य और गैर पेटेंट योग्य आविष्कारों के पहलू पर भारत और पेटेंट अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे अधिनियम 1970 के रूप में संदर्भित किया गया है) के संदर्भ में चर्चा की गई है।
यह अधिनियम, 1970 दो समितियों, बख्शी टेकचंद समिति और न्यायमूर्ति राजगोपाल अयंगर समिति के सुझावों का प्रत्यक्ष परिणाम था। समितियों की विभिन्न सिफारिशों में खाद्य और दवा से संबंधित पेटेंट, अनिवार्य लाइसेंसिंग और संबंधित कार्य आवश्यकताएं शामिल थीं जो विशेष रूप से भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर केंद्रित थीं। दवा उद्योग के लिए पेटेंट कानून का सबसे उल्लेखनीय लाभ इसके अनन्य अधिकारों का प्रावधान था, जिसने दवा विकास में नवाचार और निवेश का महत्वपूर्ण समर्थन किया, जिसके कारण भारतीय कंपनियों ने विश्व स्तर पर दवाओं का निर्यात करना शुरू किया।
पेटेंट योग्य और गैर पेटेंट योग्य आविष्कारों के बारे में समझ इकट्ठा करने के लिए, हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि ‘पेटेंट’ से हमारा क्या मतलब है।
पेटेंट का अर्थ
पेटेंट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है, जिसे एक विशेष अधिकार के रूप में समझा जा सकता है जो सरकार द्वारा किसी उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माता को दिया जाता है। उत्पाद या प्रक्रिया प्रकृति में नवीन होना चाहिए, एक समस्या का एक नया तकनीकी समाधान होना चाहिए।
डब्ल्यूआई.पी.ओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) के अनुसार, “एक पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। पेटेंट आविष्कारकों को उनके आविष्कारों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करके लाभान्वित करते हैं।”
कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, एक पेटेंट “किसी विशेष संख्या में वर्षों के लिए आविष्कार करने या बेचने का आधिकारिक कानूनी अधिकार है।”
अफाली दवा लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (1989) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पेटेंट को कुछ विशेषाधिकार, संपत्ति या अधिकार के अनुदान के रूप में परिभाषित किया, जो सरकार या किसी देश के संप्रभु द्वारा एक या अधिक व्यक्तियों को दिया गया था।
एक पेटेंट एक आविष्कार को निजी संपत्ति के रूप में स्थापित करके उसकी रक्षा करने का लाभ प्रदान करता है, जिससे पेटेंट धारक को इसके उपयोग और व्यावसायीकरण पर विशेष नियंत्रण मिलता है। पेटेंट मालिक को दूसरों को उनके आविष्कार की नकल करने या उपयोग करने से रोकने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। मालिक को न केवल आविष्कार का उपयोग करने का अधिकार है, बल्कि अन्य सभी को इसका उपयोग करने या व्यावसायिक रूप से शोषण करने से रोकने का भी अधिकार है।
एक पेटेंट अनिवार्य रूप से स्वामित्व के लिए एक विशेष अधिकार का अनुदान है, हालांकि, कुछ अतिरिक्त लाभ हैं जो पेटेंट के अनुदान के बाद पेटेंटकर्ता के लिए उपलब्ध हैं जिन पर आगे चर्चा की गई है।
पेटेंट के अधिकार और लाभ
अधिनियम, 1970 की धारा 48 पेटेंटकर्ता के अधिकारों का प्रावधान करती है जो पेटेंट प्रदान किए जाने के बाद उत्पन्न होते हैं। इनमें से कुछ अधिकार और लाभ इस प्रकार दिए गए हैं:
- किसी उत्पाद या प्रक्रिया पेटेंट के मामले में, पेटेंटकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति को पेटेंटकर्ता की सहमति के बिना आविष्कार का उपयोग करने, बनाने, व्यावसायिक रूप से शोषण करने या आयात करने से रोकने का एक विशेष अधिकार मिलता है।
- पेटेंटकर्ता या उनकी कंपनी को उनकी प्रतिस्पर्धा पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। जब भी वे अपने व्यवसाय में प्रौद्योगिकी के रूप में पेटेंट आविष्कार का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, तो यह निर्विवाद रूप से उनकी बाजार शक्ति में सुधार करेगा और उन्हें दूसरों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, जब भी बाजार में कोई और अपनी पेटेंट तकनीक का उपयोग करता है, तो उन्हें उसी के लिए स्वत्व (रॉयल्टी) शुल्क मिलेगा।
- एक पेटेंट पेटेंटकर्ता को अपने आविष्कार के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करता है जब वह अपने आविष्कार को जनता के सामने प्रकट करता है। यह उसे एक प्रदर्शनी या एक व्यापार शो में जाने और दूसरों द्वारा कॉपी किए जाने के डर के बिना अपने आविष्कार को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। इससे या तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी और बिक्री में वृद्धि होगी।
- पेटेंट को लाइसेंस देकर या समनुदेशित (ऐसाइन) करके राजस्व (रेवेन्यू) का एक नया स्रोत जोड़ा जा सकता है। इसलिए, जब कोई व्यवसाय या व्यक्ति अपने आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम होता है, तो उन्हें अपने आविष्कार को कीमत के लिए दूसरों को लाइसेंस देने या समनुदेशित करने की भी अनुमति होती है। यह एक तरह से उन्हें एकाधिकार प्रदान करता है।
- यह व्यवसायों या व्यक्तियों को निवेशकों को आकर्षित करके धन जुटाने में भी मदद करता है। इसके अलावा, पेटेंट भी खरीदा और बेचा या लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। वे बैंक ऋणों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति (कोलेटरल सिक्योरिटी) के रूप में भी काम कर सकते हैं।
- प्रतियोगी के साथ लाइसेंसिंग वार्ता के दौरान एक पेटेंट का उपयोग सौदेबाजी चिप के रूप में भी किया जा सकता है। क्रॉस-लाइसेंसिंग की अवधारणा के तहत, कंपनियां दूसरे के बदले में पेटेंट लाइसेंस के अधिकारों का आदान-प्रदान करती हैं, इससे उन्हें भारी स्वतव शुल्क का भुगतान करने से बचाया जाता है। यह बातचीत और सहयोग में मदद करता है और उस पूंजी को कम करता है जो नई तकनीक हासिल करने के लिए आवश्यक होती।
पेटेंट की विषय वस्तु एक आविष्कार है, इसलिए यह समझने से पहले कि कौन से आविष्कार पेटेंट योग्य हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ‘आविष्कार’ का गठन क्या है।
आविष्कार
अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(j) ‘आविष्कार’ शब्द को परिभाषित करती है। परिभाषा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात के दायरे को रेखांकित करता है कि भारत में क्या पेटेंट कराया जा सकता है और क्या नहीं। इस धारा के अनुसार, एक आविष्कार का अर्थ है एक नया उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें एक आविष्कारशील कदम शामिल है और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम है। आविष्कार इस संदर्भ में पूर्ण नवीनता का होना चाहिए कि इसका न तो उपयोग किया गया है और न ही दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रकाशित किया गया है।

पूर्वोक्त प्रावधान के पढ़ने के आधार पर, पेटेंट के अनुदान के लिए निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं, जिन्हें नीचे समझाया गया है:
- एक नया उत्पाद या प्रक्रिया: इस पहलू को नवीनता पहलू या मानदंड भी कहा जाता है। एक सफल पेटेंट पंजीकरण की तलाश करने के लिए किसी उत्पाद या प्रक्रिया के लिए, यह कुछ नया होना चाहिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी रूप में सार्वजनिक रूप से उपयोग या खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
- एक आविष्कारशील कदम को शामिल करना: अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(ja) ‘आविष्कारशील कदम’ की परिभाषा प्रदान करती है। इसमें मौजूदा तकनीकी ज्ञान में प्रगति शामिल है या इसका आर्थिक महत्व है, या दोनों। इन पहलुओं के साथ-साथ, यह एक ऐसा कदम भी होना चाहिए जो उस व्यक्ति के सामान्य ज्ञान के भीतर नहीं है जो विशेष उद्योग में शामिल है। इस पहलू को गैर-स्पष्ट पहलू भी कहा जाता है। किसी उत्पाद या प्रक्रिया को पेटेंट कराने के लिए, यह कुछ नया होना चाहिए और उस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के ज्ञान के भीतर नहीं होना चाहिए जिसके लिए पेटेंट मांगा गया है। आविष्कार आविष्कारक की रचनात्मकता का परिणाम होना चाहिए।
- औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम: अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(ac) ‘औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम’ शब्द को एक ऐसे आविष्कार के रूप में परिभाषित करती है जिसे किसी उद्योग में बनाया या उपयोग किया जा सकता है। यह पहलू व्यावहारिक उपयोगिता पहलू है। किसी उत्पाद या प्रक्रिया को पेटेंट कराने के लिए, इसकी कुछ व्यावहारिक उपयोगिता होनी चाहिए और केवल एक सिद्धांत नहीं होना चाहिए, व्यावहारिकता में लगने में असमर्थ होना चाहिए।
दूसरी ओर, अधिनियम, 1970 की धारा 2(1)(l) ‘नए आविष्कार’ शब्द को परिभाषित करती है। इसके दो तत्व हैं:
- कोई आविष्कार या प्रौद्योगिकी जिसका किसी प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान या अपेक्षा नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में, पेटेंट की विषय वस्तु सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए या कला की स्थिति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए।
- कोई भी आविष्कार या तकनीक जिसका उपयोग दुनिया में कहीं भी पेटेंट आवेदन दाखिल करने से पहले नहीं किया गया है।
पेटेंट करने के लिए योग्यता और आविष्कार
पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत, आविष्कार और पेटेंट करने के लिए योग्यता की अवधारणाओं को विभेदित किया गया है, वे एक आविष्कार के अलग-अलग पहलुओं से निपटते हैं। इसलिए, पेटेंट के अनुदान के लिए, यह आवश्यक है कि आविष्कार ‘आविष्कार और पेटेंट के लिए योग्यता’ के दोहरे परीक्षण को पूरा करता है।
एक नवाचार जिसे आम तौर पर एक आविष्कार माना जा सकता है, अधिनियम के तहत प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार एक आविष्कार के रूप में योग्य नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई चीज अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार आविष्कार होने की शर्त को पूरा करती भी है तो उसे अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अंतर्गत यथा निर्धारित अन्य प्रतिफलों के लिए पेटेंट प्रदान करने से मना किया जा सकता है जिसमें दो प्रकार की शर्तें लागू की गई हैं।
- पहला कहता है कि विशेष नवाचारों को इस अधिनियम के तहत आविष्कार नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी ज्ञात पदार्थ या किसी पदार्थ के नए रूप की खोज मात्र से केवल गुणों का एकत्रीकरण होता है।
- दूसरा प्रावधान करता है कि, हालांकि नवाचार अधिनियम के अनुसार एक आविष्कार होने की शर्तों को पूरा करता है, इसके बावजूद इसे अन्य कारणों से पेटेंट संरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, धारा 3 की धारा 3(b) एक आविष्कार के संरक्षण को रोकती है जिसका उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत है।
पेटेंट कानून के तहत एक आविष्कार का गठन क्या है, इसके बारे में समझ हासिल करने के बाद, सवाल उठता है कि पेटेंट द्वारा सभी प्रकार के आविष्कारों को क्या संरक्षित किया जा सकता है, पेटेंट योग्य विषय वस्तु के इस पहलू पर आगे चर्चा की जाती है।
पेटेंट योग्य विषय वस्तु
भारत में, विधायिका ने आविष्कारों की एक निश्चित विस्तृत सूची प्रदान नहीं की है जिसे पेटेंट दिया जा सकता है। जब भी कोई विषय वस्तु धारा 2(1)(j) में प्रदान किए गए पेटेंट करने के लिए योग्यता के तीन गुना मानदंडों को पूरा करती है, तो वह पेटेंट संरक्षण का दावा करने के योग्य हो जाती है। हालांकि, अंतिम पंजीकरण क्षेत्र के शासी कानून के प्रावधानों के अधीन है। भारत में, अधिनियम, 1970 की धारा 3 और धारा 4 में गैर पेटेंट योग्य विषय वस्तु की एक विशेष सूची प्रदान की गई है। यह अन्य सभी आविष्कारों को पेटेंट योग्य बनाता है यदि वे नवीन हैं और एक आविष्कारशील कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग हैं।
ट्रिप्स समझौते की धारा 5 में पेटेंटों से संबंधित प्रावधान हैं और अनुच्छेद 27 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में उत्पादों अथवा आविष्कारों की प्रक्रियाओं के लिए पेटेंट प्रदान किए जा सकते हैं। हालांकि, आविष्कार नए होने चाहिए, एक आविष्कारशील कदम शामिल होना चाहिए और औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अधिनियम, 1970 के मूल प्रावधान से प्रस्थान को चिह्नित करता था, जिसने भोजन, दवाओं या दवाओं के रूप में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग करने में सक्षम पदार्थों के लिए पेटेंट को अस्वीकार कर दिया था। इनके लिए, केवल प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति दी गई थी।
अधिनियम 1970 में पेटेंट किए जा सकने वाले आविष्कारों की सूची निर्धारित नहीं की गई है, तथापि, अधिनियम, 1970 की धारा 2, 3 और 4 स्पष्ट रूप से उन आविष्कारों से संबंधित हैं जिन्हें पेटेंट प्रदान नहीं किया जा सकता है।
गैर पेटेंट योग्य विषय वस्तु के पहलू पर प्रासंगिक निर्णय के साथ आगे चर्चा की गई है।
पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत गैर पेटेंट योग्य विषय वस्तु
अधिनियम, 1970 का अध्याय 2 उन आविष्कारों से संबंधित है जिन्हें अधिनियम द्वारा पेटेंट योग्य होने से रोक दिया गया है। दूसरे शब्दों में, इस अध्याय के प्रावधानों के भीतर आने वाले आविष्कारों को पेटेंट नहीं किया जा सकता है।
पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3
अधिनियम, 1970 की धारा 3 में उन विषयों की सूची दी गई है जो अधिनियम के अनुसार आविष्कार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसलिए पेटेंट संरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं।
धारा 3 के विभिन्न प्रावधानों पर धारा की समझ बढ़ाने के लिए प्रासंगिक निर्णय के साथ विस्तार से चर्चा की गई है।
तुच्छ आविष्कार
अधिनियम, 1970 की धारा 3(a) उन आविष्कारों को पेटेंट देने से रोकती है जो तुच्छ हैं या जो एक स्पष्ट बात का दावा करना चाहते हैं या प्राकृतिक कानूनों के विपरीत हैं। एक तुच्छ आविष्कार वह है जिसका कोई उपयोग नहीं है या पेटेंट योग्य नहीं है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित कानूनों या सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ जाता है।
उदाहरण के लिए, एक मशीन जो बिना किसी इनपुट के ऊर्जा उत्पन्न करने का दावा करती है, वह तुच्छ होगी क्योंकि यह ऊर्जा के कानून या लोगों को टेलीपोर्ट करने का दावा करने वाली मशीन का खंडन करती है। एक सतत गति मशीन पेटेंट योग्य नहीं होगी क्योंकि यह ऊष्मागतिकी (थर्मोडायनामिक) के नियमों की अवहेलना करेगी।
सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत आविष्कार
अधिनियम, 1970 की धारा 3(b) उन आविष्कारों को पेटेंट देने से रोकती है जिनका प्राथमिक या इच्छित उपयोग या वाणिज्यिक (कमर्शियल) शोषण सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विपरीत हो सकता है या मनुष्यों, जानवरों या पर्यावरण के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। कोई भी आविष्कार जो मनुष्यों, जानवरों, पौधों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है या उन आविष्कारों से संबंधित है जो डकैती, मुद्रा को खिलाने, नोटों को खिलाने, धोखाधड़ी आदि के उदाहरणों में सहायता करते हैं, को सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के खिलाफ आविष्कार माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, आविष्कार जो वाणिज्यिक उद्देश्यों या आविष्कारों के लिए मानव भ्रूण (एंब्रियो) का उपयोग करते हैं जो मनुष्यों या जानवरों की आनुवंशिक (जेनेटिक) पहचान को संशोधित करते हैं या उन्हें पीड़ित करते हैं।
सिद्धांत की खोज मात्र
अधिनियम, 1970 की धारा 3(c) उन आविष्कारों के पंजीकरण पर रोक लगाती है जो वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज या एक अमूर्त सिद्धांत के निर्माण मात्र हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रमुख उदाहरणों में गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) का सिद्धांत या ऊष्मागतिकी के नियम, पाइथागोरस प्रमेय (थीओरेम), आइंस्टीन का सापेक्षता (रेलटीविटी) का सिद्धांत या न्यूटन के गति के नियम शामिल हैं। पेटेंट किए जा सकने वाले आविष्कार प्रकृति में तकनीकी होने चाहिए और तकनीकी समस्या को हल करने का इरादा होना चाहिए।
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों की खोज मात्र
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (c) उन आविष्कारों को पेटेंट देने से रोकती है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों की खोज मात्र हैं। प्रकृति में स्वाभाविक रूप से मौजूद किसी चीज की खोज को एक आविष्कार के बजाय एक खोज माना जाता है और इस प्रकार इसे पेटेंट द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, केवल एक सूक्ष्मजीव की खोज पेटेंट संरक्षण के लिए योग्य नहीं है। हालांकि, अगर इस खोज का उपयोग एक नई वस्तु या पदार्थ बनाने के लिए एक नवीन प्रक्रिया में किया जाता है, तो यह पेटेंट संरक्षण के लिए योग्य हो सकता है।
इसमें सूर्योदय, इंद्रधनुष, बवंडर, कटाव और विद्युत चुम्बकीय दालों जैसे तत्व शामिल होंगे। इसमें पौधों या जानवरों की एक प्रजाति की खोज भी शामिल होगी। ये तत्व स्वाभाविक रूप से होते हैं और मानव बुद्धि से कोई संबंध नहीं रखते हैं, इस प्रकार, यह केवल एक खोज है और आविष्कार के रूप में दावा या पेटेंट नहीं किया जा सकता है।
एक नए रूप की खोज मात्र
अधिनियम, 1970 की धारा 3(d) पहले से ही ज्ञात पदार्थ के एक नए रूप की खोज के लिए पेटेंट के अनुदान पर रोक लगाती है जिससे पदार्थ की प्रभावकारिता में वृद्धि नहीं होती है। पहले से ही ज्ञात पदार्थ के एक नए रूप की खोज केवल एक खोज है और आविष्कार नहीं है और इस प्रकार पेटेंट योग्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यह पता लगाना कि पेरासिटामोल में एनाल्जेसिक गुण होते हैं या एथिल अल्कोहल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके एंटी-नॉकिंग गुण केवल खोज हैं और आविष्कार नहीं हैं।
यदि यह पहले से ही ज्ञात प्रायोज्यता को काफी हद तक बढ़ाता है या पदार्थ के लिए एक नया उपयोग करता है, तो इसे पेटेंट के लिए माना जा सकता है।

इस धारा के तहत प्रभावकारिता अधिनियम, 1970 की धारा 3(d) के तहत वांछित या इच्छित परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करती है। प्रभावकारिता की जांच उत्पाद के कार्य, उपयोगिता अथवा प्रयोजन पर निर्भर करेगी, जो विचाराधीन है। एक दवा के मामले में जो किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करता है, प्रभावकारिता का परीक्षण केवल दवा की चिकित्सीय प्रभावकारिता होगी, जिसे स्पष्टीकरण के साथ धारा 3 (d) के तहत सख्ती से आंका जाना है, एक नए पूर्व प्रासंगिक के सभी लाभकारी गुण नहीं, लेकिन केवल वे गुण जो इससे संबंधित हैं। इसकी प्रभावकारिता को रूप में परिवर्तन माना जाता है जो उस रूप में निहित गुणों में परिवर्तन करता है, स्वयं ज्ञात पदार्थ की प्रभावकारिता में वृद्धि के रूप में योग्य नहीं हो सकता है।
इसलिए, पदार्थ को मौजूदा पदार्थ के एक नए रूप का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और अधिनियम में उल्लिखित आविष्कार के मानदंडों को पूरा करना चाहिए। इसे धारा 3 (d) के स्पष्टीकरण के तहत प्रदान किए गए उन्नत चिकित्सीय प्रभावकारिता परीक्षण को भी पूरा करना चाहिए।
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, लवण (साल्ट), एस्टर, ईथर, बहुरूप, चयापचयों (मेटाबोलिटी), शुद्ध रूप, कण आकार, आइसोमर्स, आइसोमर्स के मिश्रण, परिसरों, संयोजनों और ज्ञात पदार्थ के अन्य व्युत्पन्न को एक ही पदार्थ माना जाएगा, जब तक कि वे प्रभावकारिता के मामले में काफी भिन्न न हों। किसी भी नई संपत्ति की खोज या किसी ज्ञात पदार्थ के उपयोग का पेटेंट तब तक पेटेंट नहीं किया जाता है जब तक कि यह मूल पदार्थ की तुलना में अधिक दक्षता का न हो, इसलिए केवल वृद्धिशील नवाचार पेटेंट के दायरे में नहीं आता है।
मोनसेंटो बनाम बोमन (2013) के मामले में, कृषि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पेटेंट पर विस्तार से चर्चा की गई। अपीलकर्ता मोनसेंटो के पास एक विशिष्ट बीज के लिए पेटेंट था जो एक विशिष्ट शाकनाशी (हर्बिसाइड) के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म थी। अपीलकर्ता ने केवल एक लाइसेंसिंग समझौते के अधीन बीज बेचे, जिसके तहत किसानों को केवल फसल बेचने की अनुमति है, लेकिन इसे फिर से लगाने की नहीं।
प्रतिवादी किसान ने एक मौसम के लिए बीज का इस्तेमाल किया और अगले बागान के लिए कुछ अन्य कम खर्चीले सोयाबीन के बीज का इस्तेमाल किया। चूंकि सस्ते बीज बड़े पैमाने पर राउंडअप-तैयार सोयाबीन के साथ लगाए गए खेतों से काटे गए थे, इसलिए कई सस्ते बीजों में राउंडअप-तैयार विशेषता थी। प्रतिवादी ने बाद में खेतों में शाकनाशी को लागू किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन पौधों में राउंडअप-तैयार विशेषता है और अगले मौसम में फिर से रोपण के लिए अपने बीज बचाते हैं। इस प्रथा की खोज अपीलकर्ता ने की और उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया गया।
प्रतिवादी ने “पेटेंट समापन” की रक्षा की, जो एक पेटेंट वस्तु के खरीदार और किसी भी बाद के मालिक को वस्तु का उपयोग करने या फिर से बेचने का अधिकार देता है, लेकिन खरीदार को पेटेंट उत्पाद की नई प्रतियां बनाने की अनुमति नहीं देता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने बचाव को खारिज कर दिया और माना कि पेटेंट समापन ने बोमन की रक्षा नहीं की क्योंकि उन्होंने “एक नया उल्लंघन वस्तु” बनाया था। एक किसान जो पेटेंट बीज खरीदता है, पेटेंट धारक की अनुमति के बिना रोपण और कटाई के माध्यम से उन्हें पुन: पेश नहीं कर सकता है।
यदि हम भारत में इस निर्णय के अनुप्रयोग को देखते हैं, तो निर्णय बहुत अलग होगा। भारत ट्रिप्स समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है और इसलिए उसे अपने राष्ट्रीय पेटेंट कानून को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना पड़ा। हालांकि, जहां तक पौधों की किस्मों का संबंध है, समझौतों के अनुच्छेद 27.3 में प्रावधान है कि एक सदस्य राज्य या तो इसे पेटेंट योग्य विषय बना सकता है या इसे ‘सुई जेनेरिस’ (अपनी तरह का) प्रणाली के तहत संरक्षित कर सकता है। भारत ने एक सुई जेनेरिस प्रणाली का विकल्प चुना है और देश की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पौधे की किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम, 2001 का संरक्षण लागू किया है। इसलिए भारतीय कानून दो महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदान करता है:
- भारत में बीज और पौधों की किस्में पेटेंट योग्य नहीं हैं।
- धारा 39 “किसान के अधिकार” प्रदान करती है और किसानों को बीज फिर से बोने की अनुमति देती है।
नोट: इस कानून पर लेख में बाद में चर्चा की गई है।
नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013) के मामले में, अपीलकर्ता ने दावा किया कि उनके उत्पाद में ‘इमैटिनिब मेसाइलेट’ मुक्त आधार था, जो एक प्रसिद्ध पदार्थ था। उत्पाद इमैटिनिब मेसाइलेट के समाधान से बनाया गया था और उस समाधान से रसायन के अल्फा और बीटा के क्रिस्टलीय रूप प्राप्त किए गए थे।
इस प्रकार, उन्होंने दावा किया कि एक-चरण एकल रूप नहीं है, बल्कि एक ज्ञात पदार्थ से क्रमिक दोहरे चरण हैं और धारा 3 (d) केवल एकल-चरण की खोज पर लागू होती है। यह भी दावा किया गया था कि धारा 3 (d) में शब्द रूप के एक तुच्छ परिवर्तन पर विचार करता है और बीटा क्रिस्टलीय रूप का आविष्कार रूप का एक बड़ा परिवर्तन नहीं था।
सर्वोच्च न्यायालय ने मोनसेंटो बनाम बोमन, 2013 के मामले पर भरोसा किया, जिसमें निम्नलिखित बिंदु बताए गए थे:
- एक बार जो ज्ञात है उसकी धारणा तय हो जाने के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि दवाओं के संदर्भ में प्रभावकारिता का मतलब चिकित्सीय प्रभावकारिता होना चाहिए।
- धारा 3(d) के अधिनियमन का कारण कृषि के संरक्षण और उन औषधों के संरक्षण से संबंधित चिंताएं थीं जो पेटेंटों की सदाबहार हैं।
- चिकित्सीय प्रभावकारिता क्या है, इसकी विस्तृत परिभाषा देना संभव नहीं है और इसे तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार देखा जाना चाहिए कि क्या ज्ञान में प्रगति से चिकित्सीय प्रभावकारिता में वृद्धि होती है
- स्पष्टीकरण एक अच्छा वैधानिक मार्गदर्शक है, जिसमें कहा गया है कि एक ही अणु के बदले हुए रूप को अधिनियम, 1970 की धारा 3 (d) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के रूप में नहीं माना जाता है। यह संभव है कि कार्बनिक अणुओं के परिवर्तित रूपों में गिरावट हो सकती है जैसे कि इसे अधिक घुलनशील या थर्मोडायनामिक रूप से स्थिर बनाना, और इस तरह के परिवर्तनों से तत्व की जैव उपलब्धता में सुधार हो सकता है। हालांकि, इनमें से कोई भी विशेषता मूल आविष्कार की चिकित्सीय प्रभावकारिता को प्रभावित नहीं करती है।
- इसके अलावा, गैर-पदार्थ की प्रभावकारिता को धारा 3 (d) के तहत अयोग्यता से बचाने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए और यह वह गैर-पदार्थ होना चाहिए, जिसका नया रूप खोजा गया है।
इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इमैटिनिब मेसाइलेट का बीटा रूप न तो एक नया पदार्थ है क्योंकि यह प्रत्याशित और स्पष्ट दोनों है और न ही यह एक पदार्थ का एक नया रूप है जो काफी बढ़ी हुई प्रभावकारिता प्रदर्शित करता है। अंत में, यह आयोजित किया गया था कि नवीनता, आविष्कारशील कदम और आवेदन के परीक्षणों के अलावा दवा पेटेंट के लिए, दावों के लिए बढ़ी हुई चिकित्सीय प्रभावकारिता का एक नया परीक्षण है जो मौजूदा दवाओं में वृद्धिशील परिवर्तनों को शामिल करता है जो नोवार्टिस की दवा भी योग्य नहीं थी।
ग्लोकेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड (2009) के मामले में, चर्चा किया गया मुद्दा पेटेंट के उल्लंघन और पेटेंट के अनुदान के लिए मानक से संबंधित था। अपीलकर्ता, ग्लोकेम इंडस्ट्रीज, के पास एक दवा उत्पाद के संबंध में पेटेंट था। विचाराधीन पेटेंट एक दवा का एक विशिष्ट सूत्रीकरण था।
प्रतिवादी पर उपरोक्त पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। तय किया जाने वाला प्रश्न यह था कि क्या प्रतिवादी का सूत्रीकरण उल्लंघन का गठन करने के लिए पर्याप्त रूप से समान था। प्रतिवादी ने अपने बचाव में अपीलकर्ता के पेटेंट की पेटेंट करने के लिए योग्यता को चुनौती दी।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के पेटेंट की वैधता को डिकोड करने के लिए नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक अनुप्रयोग के आधार पर पेटेंट की जांच की और क्या प्रतिवादी का उत्पाद पेटेंट के दायरे में आता है।
मामले में ‘तुल्यता (इक्विवेलेंट) के सिद्धांत’ की अवधारणा पर चर्चा की गई थी। शाब्दिक उल्लंघन पाया जा सकता है यदि एक अभियुक्त का उपकरण या विधि पूरी तरह से दावा किए गए दावों के दायरे में आता है, एक बार ठीक से समझा जाता है, लेकिन कोई शाब्दिक उल्लंघन नहीं है यदि कोई दावा सीमा अभियुक्त के उपकरण या विधि से अनुपस्थित है।
जब शाब्दिक उल्लंघन मौजूद नहीं होता है, तो उल्लंघन, कुछ सीमित परिस्थितियों में, फिर भी न्यायिक रूप से बनाए गए सिद्धांत के तहत पाया जा सकता है जिसे “तुल्यता का सिद्धांत” कहा जाता है।
सिद्धांत के तहत, एक उत्पाद या प्रक्रिया जो पेटेंट दावे की व्यक्त शर्तों का शाब्दिक उल्लंघन नहीं करती है, फिर भी उल्लंघन करने के लिए पाया जा सकता है यदि अभियुक्त उत्पाद या प्रक्रिया के तत्वों और पेटेंट आविष्कार के दावा किए गए तत्वों के बीच ‘तुल्यता’ है।
तुल्यता का सिद्धांत एक उल्लंघन कार्रवाई के संदर्भ में उत्पन्न होता है। यदि कोई अभियुक्त उत्पाद या प्रक्रिया सचमुच पेटेंट आविष्कार का उल्लंघन नहीं करती है, तो अभियुक्त उत्पाद या प्रक्रिया को तुल्यता के सिद्धांत के तहत उल्लंघन करने के लिए पाया जा सकता है। एक जांच के पीछे आवश्यक उद्देश्य है, क्या अभियुक्त उत्पाद या प्रक्रिया में पेटेंट आविष्कार के प्रत्येक दावा किए गए तत्व के समान या समकक्ष तत्व शामिल हैं।
तुल्यता का निर्धारण करने में, विशिष्ट पेटेंट दावे के संदर्भ में प्रत्येक तत्व द्वारा निभाई गई भूमिका का विश्लेषण इस प्रकार जांच को सूचित करेगा कि क्या एक स्थानापन्न तत्व दावा किए गए तत्व के कार्य, तरीके और परिणाम से मेल खाता है, या क्या विकल्प दावा किए गए तत्व से काफी अलग भूमिका निभाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि कैडिला के उत्पाद ने ग्लोकेम के पेटेंट का शाब्दिक या समकक्ष उल्लंघन नहीं किया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि कैडिला द्वारा सूत्रीकरण ग्लोकेम के पेटेंट फॉर्मूलेशन से काफी अलग था, इस प्रकार, उल्लंघन का गठन नहीं किया।
केवल मिश्रण
अधिनियम, 1970 की धारा 3(e) में घोषणा की गई है कि केवल घटकों के मिश्रण से किसी पदार्थ की खोज केवल संपत्तियों के एकत्रीकरण के लिए गैर पेटेंट योग्य है। मिश्रण के संयोजन का मात्र कार्य पेटेंट योग्य नहीं है जब तक कि यह एक सहक्रियात्मक प्रभाव के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। एक सहक्रियात्मक प्रभाव का अर्थ है कि दो या दो से अधिक पदार्थों की बातचीत व्यक्तिगत प्रभावों के योग से अधिक संयुक्त प्रभाव पैदा करती है।
केवल पुनर्व्यवस्था
अधिनियम, 1970 की धारा 3(f) में कहा गया है कि एक दूसरे से स्वतंत्र तरीके से काम करने वाले उपकरणों की केवल व्यवस्था या पुनर्व्यवस्था या दोहराव के कारण हुई खोज एक आविष्कार नहीं है। किसी चीज़ पर सरल सुधार या पहले से ज्ञात तत्वों का संयोजन पेटेंट योग्य नहीं है जब तक कि इसका परिणाम नया न हो या एक नवीन लेख न हो।
कृषि या बागवानी से संबंधित तरीके
अधिनियम, 1970 की धारा 3(h) इस आधार पर चर्चा करती है। जब पेटेंट करने के लिए योग्यता की बात आती है तो कृषि और बागवानी से संबंधित तरीकों की खोज विशिष्ट प्रतिबंधों का सामना करती है। उनकी पेटेंट करने के लिए योग्यता पर निषेध का मुख्य कारण यह है कि उन्हें अक्सर “अमूर्त विचारों” या “प्राकृतिक घटनाओं” श्रेणियों का विस्तार माना जाता है, जो पेटेंट योग्य नहीं हैं। पेटेंट प्रणाली का उद्देश्य आमतौर पर तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करना है जिसमें प्राकृतिक कानूनों या बुनियादी सिद्धांतों की खोजों के बजाय नए और आविष्कारशील कदम शामिल हैं।
हालाँकि, कृषि से संबंधित कुछ आविष्कार हैं जो पेटेंट योग्य हो सकते हैं:
-
जैव प्रौद्योगिकी विकास
आनुवंशिक (जेनेटिक) रूप से संशोधित जीवों (जीएमओ) या पौधों के नए उपभेदों जैसे नवाचार जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी के तरीके शामिल हैं, पेटेंट योग्य हो सकते हैं यदि वे नवीनता, आविष्कारशील कदम और औद्योगिक प्रयोज्यता के मानदंडों को पूरा करते हैं।
-
कृषि मशीनरी और उपकरण
नई कृषि मशीनरी या उपकरणों से संबंधित आविष्कार जो दक्षता या कार्यक्षमता में सुधार करते हैं, पेटेंट योग्य हो सकते हैं, बशर्ते उनमें तकनीकी नवाचार शामिल हो।
-
नवीन योग और रचना
कृषि में उपयोग किए जाने वाले नए रासायनिक योगों या रचनाओं (जैसे उर्वरक (फर्टिलाइजर), कीटनाशक, या शाकनाशी) से जुड़े तरीके पेटेंट योग्य हो सकते हैं यदि वे तकनीकी समस्या का एक नवीन और गैर-स्पष्ट समाधान प्रदान करते हैं।
डेको वर्ल्डवाइड पोस्ट हार्वेस्ट होल्डिंग बनाम पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक, (2023) के मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1970 की धारा 3(h) और धारा 3(i) के तहत विषय वस्तु के भेदभाव पर चर्चा की।
पेटेंट प्रदान करने का प्रश्न ब्लैक सिगाटोका के लिए कवकनाशी (फंगिसिडल) उपचार के आविष्कार के संबंध में था, जो केले के पौधों में एक विशिष्ट कवक के कारण होने वाले पत्तियों के धब्बे जैसे रोग का उपचार है। यह दावा किया गया था कि आविष्कार एक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका था जो प्रतिरोध के जोखिम को कम करता है और पौधे के स्वास्थ्य और उपज में सुधार करता है, जिससे इसका आर्थिक मूल्य बढ़ जाता है। पेटेंट नियंत्रक ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि आविष्कार कृषि का एक तरीका था। जबकि अपीलकर्ता का दावा है कि यह पौधों के उपचार की एक प्रक्रिया है ताकि उन्हें बीमारी से मुक्त किया जा सके।
अदालत ने कहा कि अधिनियम, 1970 की धारा 3(h) और 3(i) आविष्कार की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करती है जहां धारा 3(h) बागवानी में कृषि की एक विधि है। यह पौधों के उपचार पर विचार नहीं करता है ताकि उन्हें बीमारियों से मुक्त किया जा सके। जबकि, धारा 3 (i) उपचार और रोकथाम की प्रक्रिया से संबंधित है। अदालत ने आगे कहा कि 2002 के संशोधन द्वारा, धारा 3 (i) से ‘या पौधे’ शब्द को हटा दिया गया था।

मूल रूप से पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत धारा 3 (i) में कहा गया है कि “औषधीय, सर्जिकल, उपचारात्मक, रोगनिरोधी नैदानिक (डाग्नोस्टिक), चिकित्सीय या मनुष्यों के अन्य उपचार के लिए कोई प्रक्रिया या जानवरों या पौधों के समान उपचार के लिए कोई प्रक्रिया उन्हें बीमारी से मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए।
2002 के संशोधन के बाद, इसे बदल दिया गया, “औषधीय, सर्जिकल, उपचारात्मक, रोगनिरोधी नैदानिक, चिकित्सीय या मनुष्यों के अन्य उपचार के लिए कोई भी प्रक्रिया या जानवरों के समान उपचार के लिए कोई भी प्रक्रिया उन्हें बीमारी से मुक्त करने या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए।
परिणामस्वरूप, अधिनियम, 1970 की धारा 3 (i) का दायरा और कम हो गया है। नियंत्रक द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है कि आविष्कार कृषि की श्रेणी में धारा 3 (h) के अंतर्गत क्यों आता है। अधिनियम की धारा 3 (i) से यह स्पष्ट है कि पौधों का उपचार गैर पेटेंट करने के लिए योग्यता के दायरे में नहीं आएगा। अदालत ने नियंत्रक के आदेश को रद्द कर दिया और अदालत द्वारा स्पष्ट किए गए कानून पर पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेज दिया।
मनुष्यों और जानवरों के उपचार से संबंधित आविष्कार
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (i) में कहा गया है कि मनुष्यों या जानवरों में बीमारियों के इलाज के लिए औषधीय, उपचारात्मक, रोगनिरोधी, नैदानिक, चिकित्सीय प्रक्रिया की खोज पेटेंट योग्य नहीं है। यदि पेटेंट कराया जाता है तो उपचार प्रक्रिया डॉक्टरों को रोगियों के लिए सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने से रोकेगी। पेटेंट देखभाल के बिंदु पर चिकित्सा चिकित्सकों को प्रतिबंधित करेगा। जानवरों के लिए उपचार के मामले में जो उनके स्वास्थ्य को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, या उनके आर्थिक मूल्य या उनके उत्पादों को बढ़ाना भी पेटेंट योग्य नहीं हैं। इसमें मौखिक या इंजेक्शन योग्य दवा, सिलाई मुक्त सर्जरी, और सजीले टुकड़े (प्लॉक) जैसी स्थितियों के लिए उपचार जैसे तरीके शामिल हैं, जो आविष्कार के रूप में योग्य नहीं हैं।
आविष्कार के रूप में पशु और पौधे
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (j) सूक्ष्मजीवों को छोड़कर पौधों या बीजों के लिए पेटेंट के अनुदान पर रोक लगाती है, जिसमें उनके प्रसार के लिए जैविक प्रक्रियाएं, जानवरों और उनके उत्पादन या लंबे समय तक जैविक प्रक्रियाएं शामिल हैं। पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से पाई जाने वाली किसी चीज को पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। कोई बस एक नए पौधे की खोज नहीं कर सकता है और पेटेंट संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है।
भारत में पौधों की किस्मों या उत्पादों पर पेटेंट रखना भी संभव नहीं है। अधिनियम, 1970 यह स्पष्ट करता है कि बीजों, किस्मों और प्रजातियों सहित पूरे या आंशिक रूप से पौधे और पौधों के उत्पादन या प्रसार के लिए अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाएं पेटेंट योग्य आविष्कार नहीं हैं।
भारत सरकार ने ‘सुई जेनेरिस’ (अपनी तरह की) प्रणाली को अपनाते हुए पौधे की किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम, 2001 (पीपीवीएफआर) अधिनियमित किया। भारतीय विधान न केवल पौधों की नई किस्मों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1978 के अनुरूप है बल्कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की प्रजनन संस्थाओं और किसानों के हितों की रक्षा के लिए भी पर्याप्त प्रावधान हैं। यह कानून पादप प्रजनन गतिविधि में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है और ट्रिप्स के प्रावधानों को इस तरह से लागू करता है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों और अनुसंधान संस्थानों के साथ-साथ संसाधन-विवश किसानों सहित सभी हितधारकों के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक हितों का समर्थन करता है।
पीपीवीएफआर अधिनियम 2001 के अनुसार, “एक किसान को इस अधिनियम के तहत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपने कृषि उपज को बचाने, उपयोग करने, बोने, विनिमय, साझा करने या बेचने का अधिकार है, जैसा कि वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले हकदार था: बशर्ते कि किसान इस अधिनियम के तहत संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज बेचने का हकदार नहीं होगा। इसे किसानों और प्रजनकों दोनों के अधिकारों पर विचार करने वाला दुनिया का पहला अधिनियम माना जाता है।
तथापि, अधिनियम के अंतर्गत नई पौध किस्मों के पंजीकरण की अनुमति है। अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि नई किस्म नवीन, विशिष्ट, एकसमान और स्थिर होनी चाहिए।
- नवीन: ऐसी नई किस्म के कटे हुए उत्पाद को प्रजनक या उनके उत्तराधिकारी की सहमति से भारत में एक वर्ष से पहले और भारत के बाहर चार साल से पहले बेचा नहीं जाना चाहिए, लेकिन पेड़ों और लताओं के मामले में छह साल से पहले।
- स्पष्टतया भिन्न: कम से कम एक आवश्यक विशेषता होनी चाहिए जो नई किस्म को स्पष्ट रूप से एक किस्म से अलग करती है जो किसी भी देश में सामान्य ज्ञान का विषय है।
- एकरूप: नई किस्म की आवश्यक विशेषताओं को किसी भी भिन्नता के अधीन पर्याप्त रूप से समान रहना चाहिए जो इसके प्रसार की विशेष विशेषताओं से उम्मीद की जा सकती है।
- स्थिर: किस्म के बार-बार प्रसार के बाद भी, इसकी आवश्यक विशेषताएं समान रहनी चाहिए।
गणितीय, व्यावसायिक तरीके या कंप्यूटर प्रोग्राम
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (k) इस आधार पर चर्चा करती है। अधिनियम के अनुसार, कोई भी गणितीय गणना या वैज्ञानिक सत्य या कोई कार्य, मानसिक कौशल या व्यवसाय, विधियों या एल्गोरिदम से संबंधित गतिविधियां पेटेंट संरक्षण के लिए अयोग्य हैं।
रेथियॉन कंपनी बनाम पेटेंट महानियंत्रक (2023) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सेट-अप में शेड्यूलिंग से संबंधित एक आविष्कार से संबंधित प्रश्न पर चर्चा की, जिसमें कंप्यूटर प्रणाली और नेटवर्क में पाए जाने वाले सभी प्रकार के हार्डवेयर डिवाइस शामिल हैं।
अदालत ने कहा कि धारा 3(k) उन मामलों की पेंटिंग निर्धारित करती है जो धारा में उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं और इस मामले में, आविष्कार गणितीय व्यवसाय पद्धति या एल्गोरिथ्म से संबंधित नहीं है। तथापि, क्या यह स्वत कम्प्यूटर प्रोग्राम की श्रेणी से संबंधित है, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए।
कंप्यूटर प्रोग्राम के संदर्भ में 2017 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों की पहचान के लिए परीक्षण संकेतक प्रकाशित किए गए थे। दिशानिर्देश कंप्यूटर से संबंधित आविष्कारों की पेटेंट करने के लिए योग्यता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। ऐसे आवेदनों की जांच करते समय पेटेंट कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और इस क्षेत्र में विकसित हुए न्यायशास्त्र पर भी चर्चा की गई है।
एक सॉफ्टवेयर नवाचार के लिए पेटेंट प्राप्त करने के लिए, नवाचार को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि जिस नवाचार को संरक्षित करने की मांग की जाती है उसमें विषय वस्तु शामिल हो जो “केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है”। इसलिए, भारत में एक सॉफ्टवेयर आविष्कार के लिए एक पेटेंट प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते सॉफ्टवेयर आविष्कार हार्डवेयर के साथ संयोजन के रूप में पेटेंट योग्य हो। यह वास्तव में आविष्कारकों के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
अधिनियम, 1970 की धारा 3(k) के तहत ‘प्रति से’ शब्दों का उपयोग बताता है कि परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि कभी-कभी कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ अन्य चीजें शामिल होती हैं जो सहायक होती हैं या अपना स्वयं का विकास करती हैं और विधायिका का इरादा उन्हें अपने आविष्कारों के पेटेंट के अनुदान से अस्वीकार करना नहीं है, हालांकि, इस तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम को पेटेंट दिए जाने का इरादा नहीं है।
अदालत ने यह भी माना कि नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्थाओं में, जहां अधिकांश आविष्कार कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित होते हैं, यह तर्क देना अनुचित होगा कि ऐसे सभी आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं हैं। कृत्रिम बौधिमत्ता, ब्लॉकचेन प्रद्योगिकी, वगैरह के क्षेत्र में नवाचार कंप्यूटर प्रोग्राम पर आधारित हैं और यह दावा करने के लिए कि वे केवल इस कारण से पेटेंट योग्य नहीं होंगे, मनमाना है कि ऐसा उत्पाद देखना दुर्लभ है जो कंप्यूटर प्रोग्राम, कारों या अन्य ऑटोमोबाइल, माइक्रो वाशिंग मशीन, वगैरह पर आधारित नहीं है। सभी के पास किसी न किसी प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया है। इसलिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित ऐसे कार्यक्रमों का उत्पादन करने वाला प्रभाव पेटेंट करने के लिए योग्यता के परीक्षण को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
कहने के लिए शब्द को शामिल किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर विकसित किए गए वास्तविक आविष्कारों को पेटेंट से इनकार नहीं किया जाता है। अदालत ने अंत में महानियंत्रक को अदालत के निर्णय के संदर्भ में आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया।
यूपीआई ढांचे की पेटेंट के लिए योग्यता
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई को दो पहलुओं के संदर्भ में समझा जा सकता है। पहला एक अवधारणा या प्रणाली के रूप में स्वयं विधि है और दूसरा यूपीआई से संबंधित विशिष्ट नवाचार या अद्वितीय तकनीकी कार्यान्वयन है। जबकि पहला आमतौर पर पेटेंट योग्य नहीं होता है, बाद वाले को पेटेंट कराया जा सकता है।
एक विचार के रूप में यूपीआई विधि इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे ट्रांसफर करने की अवधारणा पर बनाई गई है। यह केवल एक अमूर्त विचार या मौलिक आर्थिक अभ्यास है और इसलिए पेटेंट योग्य नहीं है। इसके अलावा, यूपीआई भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानक है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित किया गया है। यह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और बड़े पैमाने पर लोगों के लिए सुलभ है, इसलिए एक पेटेंट के अनुदान की आवश्यकताएं जो नयापन और गैर-स्पष्ट नवाचार है, गायब हैं।
हालांकि, अगर किसी व्यक्ति ने यूपीआई ढांचे के भीतर एक अद्वितीय, नवीन तकनीकी नवाचार या एल्गोरिदम बनाया है जो मानक सूत्र में नहीं पाया जाता है, तो यह पेटेंट योग्य है। उदाहरण के लिए, लेनदेन सुरक्षा में सुधार के लिए एक नवीन विधि या भुगतान अनुरोधों को संभालने के लिए एक अद्वितीय एल्गोरिथ्म पेटेंट योग्य हो सकता है यदि वे नवीनता, गैर-स्पष्टता और उपयोगिता के मानदंडों को पूरा करते हैं।
विशिष्ट तकनीकी सुधारों के मामले में जो इसके प्रदर्शन या सुरक्षा में सुधार करते हैं। इसके अलावा, यदि कुछ सॉफ्टवेयर नवाचार व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं जो लेनदेन डेटा के प्रबंधन या उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार के संदर्भ में इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। उन नवाचारों को पेटेंट योग्य किया जा सकता है।
निष्कर्ष निकालने के लिए, यूपीआई भुगतान प्रणाली समग्र रूप से पेटेंट योग्य नहीं है। हालांकि, विशिष्ट, नवीन और तकनीकी नवाचार संभावित रूप से पेटेंट योग्य हो सकते हैं।
कॉपीराइट योग्य विषय वस्तु
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (l) इस आधार पर चर्चा करती है। इसके अनुसार, साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य जिसमें सिनेमैटोग्राफिक और टेलीविजन प्रोडक्शन सहित कोई अन्य सौंदर्यपरक रचना शामिल है, एक आविष्कार नहीं है। लेखन, पेंटिंग, संगीत रचनाएं या सिनेमैटोग्राफिक प्रस्तुतियों जैसी गतिविधियां पेटेंट योग्य नहीं हैं। तथापि, इनमें से कुछ को, यदि वे शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है।
मानसिक कार्य या खेल खेलने की विधि
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (m) घोषित करती है कि एक नवाचार जो केवल एक योजना या नियम या मानसिक कार्य करने की विधि या खेल खेलने की विधि है, एक आविष्कार नहीं है और इस तरह पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। शतरंज या सुडोकू जैसे खेल खेलने की रणनीतियाँ तकनीकी हस्तक्षेप के बजाय मानसिक अभ्यास हैं, और इस तरह, वे पेटेंट संरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं।

जानकारी की प्रस्तुति
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (n) इस आधार पर चर्चा करती है। इसमें कहा गया है कि जानकारी प्रस्तुत करने के तरीके, जैसे कि टेबल, चार्ट, पाई चार्ट या ग्राफ़ के रूप में, आविष्कार नहीं माना जाता है और इसलिए पेटेंट योग्य नहीं हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि डेटा को व्यवस्थित करने या प्रदर्शित करने के मूलभूत तरीकों को पेटेंट संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन्हें आम तौर पर तकनीकी नवाचारों के बजाय संचार के लिए उपकरण माना जाता है। एक कंपनी के लिए वार्षिक बिक्री के आंकड़ों पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तालिका, समय के साथ विभिन्न शहरों की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने वाला एक बार चार्ट, और कई वर्षों में शेयर बाजार की कीमतों में रुझानों को दर्शाने वाला एक लाइन ग्राफ कुछ उदाहरण हैं।
एकीकृत परिपथों (सर्किट) की स्थलाकृति (टोपोग्राफी)
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (o) इस आधार पर चर्चा करती है। यह एक नवाचार के पंजीकरण को रोकता है जो केवल एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति से संबंधित है।
पारंपरिक ज्ञान
अधिनियम, 1970 की धारा 3 (p) में घोषणा की गई है कि एक नवाचार जो केवल पारंपरिक रूप से ज्ञात घटकों के ज्ञात गुणों का पारंपरिक ज्ञान या दोहराव है, अधिनियम के तहत आविष्कार नहीं है और इस प्रकार पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान या कौशल ज्ञान और कौशल हैं जो एक समुदाय में पीढ़ियों को पास किए जाते हैं। ये पहले से ही प्रसिद्ध हैं और इनमें नवीनता का तत्व नहीं है। इसलिए, इनका पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण, नीम के एंटीसेप्टिक गुण आदि।
पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 4
धारा 4 परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कारों से संबंधित है जो पेटेंट योग्य नहीं हैं और जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 (1) के अंतर्गत आते हैं।
अधिनियम, 1970 की धारा 65 केंद्र सरकार को पेटेंट रद्द करने के लिए पेटेंट नियंत्रक को निर्देश देने का अधिकार देती है। ऐसी शक्तियों का प्रयोग तब किया जा सकता है जब केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित आविष्कार के लिए पेटेंट दिया गया है जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 20 के अनुसार नहीं है। महानियंत्रक को पेटेंटकर्ता को नोटिस देने की आवश्यकता होती है, और उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद, पेटेंट को रद्द कर सकता है।
दवा उद्योग के क्षेत्र में पेटेंट देने का सवाल अक्सर विवादों में घिर जाता है, इसलिए अगले खंड में, हम इस विषय पर भारतीय स्थिति के विकास को देखेंगे।
दवा उद्योगों में उत्पाद पेटेंट की पेटेंट के लिए योग्यता
भारत की स्वतंत्रता के समय, भारतीय पेटेंट कानून पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 द्वारा शासित होता था जो उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट दोनों के लिए प्रदान करता था। हालांकि, बाद में सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तुत पेटेंट कानून ने भारतीयों की तुलना में विदेशियों को अधिक लाभान्वित किया है। इसने देश के भीतर वैज्ञानिक अनुसंधान (रिसर्च) और औद्योगीकरण को बढ़ावा नहीं दिया और इसके बजाय नवाचार और आविष्कारशीलता पर अंकुश लगाया।
परिणामस्वरूप, पेटेंट कानून की समीक्षा टेकचंद समिति और अय्यंगार समिति द्वारा की गई थी। इस समिति ने कहा कि रासायनिक पदार्थों और खाद्य और दवा से संबंधित आविष्कारों के लिए पेटेंट केवल प्रदान किया जाना चाहिए, प्रक्रिया, पेटेंट और उत्पाद पेटेंट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इसके बाद, समितियों की सिफारिश पर 1970 का पेटेंट अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसने पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 को बदल दिया। अधिनियम, 1970 की धारा 5 में उन पदार्थों के लिए उत्पाद पेटेंट को बाहर रखा गया था जो खाद्य या दवा या दवाओं में उपयोग किए जाने के लिए आशयित या सक्षम थे। इससे भारत के दवा उद्योग पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। दवाओं के उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत दुनिया में कम कीमत वाली जेनेरिक दवाओं का निर्यातक बन गया।
तत्पश्चात्, टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते (जीएटीटी) के अंतर्गत उरुग्वे दौर की वार्ताएं आयोजित की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ और बाद में 1995 में ट्रिप्स समझौता तैयार हुआ। ट्रिप्स समझौता एक व्यापक बहुपक्षीय समझौता था जिसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया था और इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर आई.पी. कानूनों को सुसंगत बनाना था।
चूंकि हम विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं इसलिए भारत ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत दायित्वों से भी बंधा हुआ है। ट्रिप्स समझौते के अनुसार, भारत को दवा और कृषि रासायनिक पदार्थों के क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट के अनुदान की अनुमति देने की आवश्यकता थी, जिसे पहले 1970 अधिनियम की धारा 5 के तहत रोक दिया गया था।
नतीजतन, भारत सरकार 1994 में पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश लाई, जिसने किसी पदार्थ के लिए एक आविष्कार के पेटेंट के लिए दावे की अनुमति देने के लिए प्रदान किया, जिसका उपयोग दवा या दवा के रूप में उपयोग करने में सक्षम था और उस उत्पाद के संबंध में विशेष विपणन अधिकार प्रदान करने के लिए जो इस तरह के पेटेंट दावे का विषय है।
1999 में, पेटेंट अधिनियम, 1970 में संशोधन किया गया और अध्यादेश के अनुरूप लाया गया। 2004 में, सरकार पेटेंट संशोधन अध्यादेश लाई जिसके द्वारा अधिनियम, 1970 की धारा 5 को हटा दिया गया, जिसने अन्य आविष्कारों के साथ दवा उत्पादों के पेटेंट के लिए दरवाजे खोल दिए।
जब संसद में इस विधान पर चर्चा हुई तो अध्यादेश को विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। कुछ चिंताओं को उठाया गया था जैसे कि दवा और कृषि क्षेत्रों में पेटेंट उत्पादन। रासायनिक उत्पादों का जीवन रक्षक दवाओं को कुछ लोगों की पहुंच से बाहर रखने का प्रभाव होगा।
इसलिए, कानून को देश के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य के साथ-साथ संधि के तहत अपने दायित्व के बीच संतुलन बनाना था। लोगों की आशंकाओं को संतुलित करने के लिए, संसद ने 1970 अधिनियम की धारा 3 (d) में संशोधन किया, जिसका उद्देश्य दवा और कृषि, रासायनिक पदार्थ उद्योगों में उत्पाद पेटेंट के किसी भी दुरुपयोग का ख्याल रखना था।
रसायन और दवा उद्योग में एक नए उत्पाद का मतलब जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल नया या पूरी तरह से अपरिचित हो या पहले मौजूद न हो। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो पिछले उत्पाद से अलग है जो पहले मौजूद उत्पाद से बेहतर है, जो उसी तरह के दूसरे उत्पाद के अलावा है।
इस प्रकार, रसायनों और दवा के मामले में, यदि जिस उत्पाद पर पेटेंट उत्पाद संरक्षण लागू किया जाता है, वह गैर-प्रभावकारिता के साथ पहले से ही ज्ञात पदार्थ का एक नया रूप है, तो उत्पाद को दिए जाने के लिए, एक पेटेंट को धारा 2(1) (j) और (ja) के तहत प्रदान किए गए आविष्कार का परीक्षण, स्पष्टीकरण के साथ पढ़ी गई धारा 3(d) में प्रदान की गई बढ़ी हुई प्रभावकारिता का परीक्षण।
अधिनियम की धारा 3 (d) पेटेंट करने के लिए योग्यता की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है, जो आविष्कार शब्द से अलग है।
कृत्रिम बौद्धिमत्ता का क्षेत्र हाल के दिनों में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, यह अनिवार्य रूप से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। सिरी जैसे आभासी सहायकों के उपयोग से लेकर चैटजीपीटी जैसे सॉफ़्टवेयर के उपयोग तक, हम धीरे-धीरे अपने जीवन में ए.आई. के एकीकरण को देख सकते हैं। इसलिए, ए.आई. से जुड़े आविष्कारों की पेटेंट करने के लिए योग्यता पर चर्चा करना उचित हो जाता है।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) (ए.आई.) की पेटेंट करने के लिए योग्यता
ए.आई. से संबंधित पेटेंट ए.आई. प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं को कवर कर सकते हैं। य़े हैं:
- एल्गोरिदम और तरीके: ए.आई. से संबंधित पेटेंट में मशीन लर्निंग, तंत्रिका नेटवर्क या डेटा प्रसंस्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट एल्गोरिदम शामिल होंगे।
- अनुप्रयोगों: ए.आई. से संबंधित पेटेंट में ए.आई. के व्यावहारिक उपयोग शामिल होंगे, जैसे छवि पहचान, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या सिफारिश प्रणाली।
- प्रणाली और वास्तुकला: ए.आई. से संबंधित पेटेंट में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन शामिल होंगे जो ए.आई. तकनीक को लागू करते हैं, जिसमें विशेष प्रोसेसर शामिल हैं।
- प्रक्रियाएं और तकनीकी जानकारी: ए.आई. मॉडल को प्रशिक्षित करने या उनके प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए नवीन तरीके।
ए.आई. की पेटेंट करने के लिए योग्यता को तीन दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है:
ए.आई. प्रणाली का पेटेंट
संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपीय संघ में, ए.आई. प्रणाली को पेटेंट कराया जा सकता है यदि वे पेटेंट करने के लिए योग्यता की तीन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं आविष्कार की नवीनता या नएपन, आविष्कारशील कदम या आविष्कार की गैर-स्पष्टता और औद्योगिक प्रयोज्यता की आवश्यकता हैं। हालाँकि, ए.आई. एल्गोरिदम या ए.आई. से संबंधित अमूर्त विचार पेटेंट योग्य नहीं हैं। बल्कि उन एल्गोरिदम के विशिष्ट अनुप्रयोग या कार्यान्वयन का पेटेंट कराया जा सकता है।
ए.आई. एल्गोरिदम की पेटेंट करने के लिए योग्यता
ए.आई. के बारे में एक विशुद्ध रूप से गणितीय एल्गोरिथ्म या एक अमूर्त सिद्धांत या विचार पेटेंट योग्य नहीं है। हालांकि, अगर एल्गोरिथ्म व्यावहारिक रूप से लागू होता है तो यह हो सकता है। इसका एक उदाहरण चिकित्सा स्थितियों के निदान या विनिर्माण प्रक्रियाओं के अनुकूलन के लिए ए.आई.-आधारित विधि होगी जिसे पेटेंट कराया जा सकता है यदि यह एक नवीन और गैर-स्पष्ट तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है।
एक आविष्कारक के रूप में ए.आई.
स्थिति अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या ए.आई. प्रणाली को पेटेंट अनुप्रयोगों में आविष्कारक के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। विश्व स्तर पर, वर्तमान स्थिति केवल मनुष्यों को आविष्कारक के रूप में स्वीकार करती है। हालांकि, तकनीकी प्रगति की तीव्र गति को देखते हुए, यह वास्तव में भविष्य में एक वास्तविकता बन सकता है।
पेटेंट योग्य और गैर पेटेंट योग्य आविष्कारों से संबंधित निर्णय
पेटेंट योग्य आविष्कार
ब्लैकबेरी लिमिटेड बनाम पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक (2024) दिल्ली उच्च न्यायालय
- तथ्य: इस मामले में, ‘स्वचालित चयन’ और ‘कैश प्रबंधक द्वारा अद्यतन’ की सुविधा के लिए पेटेंट की मांग की गई थी। इसे “संभावना के आधार पर आत्मविश्वास स्तर प्रदान करने की विशेषता” पर एक नवीन तकनीकी प्रगति के रूप में दावा किया गया था, जो कि पूर्व कला थी, जिस पर “कैश प्रबंधक द्वारा ‘स्वचालित चयन’ और अद्यतन करने की विशेषता नवीन तकनीक थी”।
पेटेंट आवेदन को पेटेंट नियंत्रक द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था कि तत्व एल्गोरिथम और कंप्यूटर प्रोग्राम हैं और इसलिए अधिनियम, 1970 की धारा 3 (k) के दायरे में आते हैं।
अपीलकर्ता द्वारा यह दावा किया गया था कि तकनीकी विशेषता जो आविष्कार का विषय है, एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसने ब्लैकबेरी को प्रचार सामग्री जारी करने के लिए प्रेरित किया, इस बात पर प्रकाश डाला कि इसके उपकरणों पर अधिक संगीत डाउनलोड किया जा सकता है, और यदि विषय आविष्कार में दावा की गई सुविधा सक्षम है, तो डिवाइस पर अधिक से अधिक संगीत या अन्य सामग्री डाउनलोड की जा सकती है। इसलिए इसे अधिनियम, 1970 की धारा 3 (k) की सीमा को पार करने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। इसके अलावा, तकनीकी प्रभाव इस तथ्य से काफी स्पष्ट है कि यह उपयोगकर्ता को कई स्रोतों के माध्यम से संगीत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो इस हस्तक्षेप से पहले संभव नहीं था।
- मुद्दा: क्या विषय वस्तु स्वतः एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और इस प्रकार अधिनियम, 1970 की धारा 3 (k) के तहत पेटेंट संरक्षण पर रोक लगा दी गई है?
- निर्णय: अदालत ने कहा कि जबकि विषय पेटेंट और आवेदन और पूर्व कला के बीच कुछ समानताएं हैं, वर्तमान पेटेंट आवेदन कई नवीन तत्वों का परिचय देता है, जो दोनों को अलग करते हैं। जबकि दोनों में उपयोगकर्ता वरीयताओं के आधार पर मीडिया फ़ाइलों का स्वचालित चयन शामिल है, वर्तमान पेटेंट विषय संभावना के आधार पर “आत्मविश्वास स्तर” का उपयोग करता है, पूर्व कला में उपयोग की जाने वाली लोकप्रियता रेटिंग की तुलना में एक अलग मेट्रिक प्रदान करता है।
इसके अलावा, वर्तमान विषय पेटेंट में आत्मविश्वास के स्तर के आधार पर मीडिया फ़ाइल को वर्गीकृत करने और चयन के लिए फ़िल्टर के रूप में उपलब्ध भंडारण के लिए फ़ाइल आकारों की तुलना करने के लिए एक विशिष्ट चरण शामिल है जो पूर्व कला में प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान पेटेंट आवेदन में एक विशिष्ट कैश प्रबंधक को शामिल करना जो चयनित मीडिया फ़ाइलों से संबंधित जानकारी वाली सूची को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार है, एक नवीन विशेषता है जो पूर्व कला में नहीं मिली है।
इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कैश प्रबंधक, विशिष्ट वर्गीकरण और फ़िल्टरिंग प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी कदम सहित ये विशिष्ट विशेषताएं पूर्व कला में प्रकटीकरण से परे एक तकनीकी अग्रिम प्रदान करती हैं और इसलिए, नवीनता की कमी के कारण गैर पेटेंट के लिए योग्यता का आधार खड़ा नहीं होता है।

बायोट्रॉन लिमिटेड बनाम पेटेंट और डिजाइन महानियंत्रक (2023) कलकत्ता उच्च न्यायालय
- तथ्य: इस मामले में, आविष्कार का विषय यौगिकों (कंपाउंड) की नवीन संरचना से संबंधित है, जिन्हें वायरल संक्रमण के इलाज और रोकथाम में प्रभावी होने का दावा किया गया था, विशेष रूप से एचआईवी, एचसीवी और डेंगू वायरस के खिलाफ। यह दावा किया गया था कि चक्रीय प्रतिस्थापन वाले यौगिक गैर-चक्रीय विकल्प वाले यौगिकों से बेहतर हैं जो अपीलकर्ता के आविष्कार से पहले मौजूद थे। इसलिए, विषय आविष्कार अन्य ज्ञात यौगिकों की तुलना में तकनीकी रूप से उन्नत है।
पेटेंट और डिजाइन के महानियंत्रक द्वारा आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इसमें अधिनियम, 1970 की धारा 2 (1) (j) और 2 (1) (ja) के तहत आविष्कारशील कदमों का अभाव था और आगे यह अधिनियम, 1970 की धारा 3 (d) के तहत एक गैर पेटेंट योग्य विषय था।
- मुद्दा: क्या विषय वस्तु में आविष्कारशील कदम का अभाव है और यह अधिनियम, 1970 की धारा 3 (d) के दायरे में भी आता है?
- निर्णय: न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता ने यह खुलासा करने के लिए पूर्व कला के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया था कि चक्रीय प्रतिस्थापन में चक्रीय प्रतिस्थापन वाले यौगिकों की तुलना में बेहतर गतिविधि है। पेटेंट की विषय वस्तु में गैर-चक्रीय प्रतिस्थापन, जिनका उक्त प्रतिजनों (एंटीजन) के विरुद्ध कोई कार्यकलाप नहीं है, की तुलना में तीन वायरल एंटीजन के विरुद्ध यौगिकों का औसत जीवाणु स्कोर होता है।
पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक द्वारा आदेश इस पहलू पर विचार करने में विफल रहा, अदालत ने नोवार्टिस एजी बनाम भारत संघ (2013) में मामले पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया था कि धारा 3 (d) स्पष्ट रूप से रासायनिक पदार्थों के लिए योग्यता मानकों का दूसरा स्तर स्थापित करती है ताकि सच्चे और वास्तविक आविष्कारों के लिए दरवाजा खुला रह सके, लेकिन एक ही समय में दोहराए जाने वाले पेटेंट के किसी भी प्रयास की जांच करने के लिए। धारा 3 (d) रसायनों और दवा पदार्थों के सभी वृद्धिशील आविष्कारों के लिए पेटेंट संरक्षण पर रोक नहीं लगाती है।
अंत में, अदालत ने पेटेंट अधिकारियों से फैसले में दिए गए निर्देशों के आलोक में अपने आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा।
गैर पेटेंट योग्य आविष्कार
विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम बनाम हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज (1979) सर्वोच्च न्यायालय
- तथ्य: इस मामले में प्रतिवादी हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज एक भागीदारी फर्म है जो पीतल और जर्मन चांदी के बर्तनों के निर्माण में कारोबार करती है। अपीलकर्ता विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम का बर्तन बनाने का व्यवसाय भी था। प्रतिवादी फर्म के भागीदारों में से एक ने बर्तनों के निर्माण के लिए एक उपकरण और विधि का आविष्कार किया, जिसने उत्पादित वस्तुओं में सुधार, सुविधा, गति, सुरक्षा और बेहतर फिनिश पेश किया। इसके बाद, उन्होंने कथित आविष्कार का पेटेंट कराया। बाद में, प्रतिवादी को पता चला कि प्रतिवादी उपकरण और विधि का उपयोग कर रहा था, जो पूर्व पेटेंट का विषय था और अपीलकर्ता के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) के लिए मुकदमा दायर किया।
अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादी के पेटेंट द्वारा कवर की गई विधि ‘खराद’ (हेडस्टॉक, एडेप्टर और टेल स्टॉक) ज्ञात है और वाणिज्यिक दुनिया में खुले तौर पर और आमतौर पर उपयोग की जाती है। इस प्रकार, आविष्कार निर्माण या सुधार का एक नया तरीका नहीं था, न ही इसमें कोई आविष्कारशील कदम शामिल था। इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।
- मुद्दा: क्या विषय वस्तु में पेटेंट के अनुदान के लिए पात्र होने के लिए एक आविष्कारशील कदम शामिल है?
- निर्णय: अदालत ने अपीलकर्ता की आपत्ति को देखते हुए कहा कि एक आविष्कार को पेटेंट योग्य बनाने के लिए, किसी ऐसी चीज पर सुधार जो पहले से ही ज्ञात है, केवल एक कार्यशाला सुधार से अधिक होना चाहिए। इसे स्वतंत्र रूप से आविष्कार या एक आविष्कारशील कदम की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। एक सुधार होने के लिए इसे एक नया परिणाम या एक नया लेख या पहले से बेहतर या सस्ता लेख उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए, प्रतिवादी का आविष्कार पेटेंट के अनुदान के लिए योग्य नहीं होगा।
ओपनटीवी आईएनसी बनाम पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक, (2023) दिल्ली उच्च न्यायालय
- तथ्य: इस मामले में अपीलकर्ता कंपनी इंटरैक्टिव टेलीविजन समाधान प्रदान करने में लगी हुई है। इसने “उपहार मीडिया प्रदान करने के लिए प्रणाली और विधि” के पेटेंट के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे “एक नेटवर्क वास्तुकला और किसी भी प्रकार के डिजिटल या मूर्त मीडिया के इंटरैक्टिव मीडिया सामग्री वितरण के आदान-प्रदान को सक्षम करने के लिए उसी पर लागू की गई विधि” कहा गया है।
आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि विषय वस्तु अधिनियम, 1970 की धारा 3 (k) के अंतर्गत आती है और इसलिए पेटेंट योग्य नहीं है।
- मुद्दा: क्या विषय अधिनियम, 1970 की धारा 3 (k) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के अंतर्गत आता है?
- निर्णय: अदालत ने कहा कि विषय वस्तु “विभिन्न ज्ञात घटकों और प्रौद्योगिकियों को इस तरह से अनुकूलित किया जा रहा है ताकि मानवीय हस्तक्षेप के बिना उपहार देने में सक्षम बनाया जा सके, सिवाय शुरुआत में जहां उपहार और प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा चुना जाता है”। इसे विभिन्न अवतार स्वरूपों में एक नेटवर्क के रूप में और विभिन्न मीडिया प्रारूपों को प्रसारित करने के उद्देश्य से भी वर्णित किया गया है। पेटेंट का अनुदान वास्तव में उपहार देने की एक विधि से संबंधित एकाधिकार होगा और चूंकि यह एक व्यावसायिक विधि है, इसलिए कोई पेटेंट नहीं दिया जा सकता है। धारा 3 (k) के अनुसार, व्यावसायिक तरीकों के संबंध में बहिष्करण एक पूर्ण है।

निष्कर्ष
हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक ज्ञान-संचालित हैं। जहां सरकारें अपने नागरिकों में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। हमें रचनात्मक और आविष्कारशील विचारों की आवश्यकता है जो या तो एक नई अवधारणा लाते हैं या मौजूदा में सुधार करते हैं। यदि कोई व्यवसाय या व्यक्ति इस तरह के उत्पाद या प्रक्रिया को विकसित करता है, तो वे आदर्श रूप से प्रौद्योगिकी पर मालिकाना अधिकार या एकाधिकार रखना चाहते हैं और दूसरों को इसका उपयोग करने से रोकना चाहते हैं।
यह वास्तव में सच है कि पेटेंट नवाचार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं लेकिन जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह यह है कि वे अस्थायी एकाधिकार भी बनाते हैं। आवश्यक प्रौद्योगिकियों तक सार्वजनिक पहुंच के साथ पेटेंटकर्ता के पेटेंट संरक्षण को संतुलित करने का कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि तकनीकी प्रगति का लाभ समाज द्वारा एक साथ साझा किया जाता है।
एक मजबूत पेटेंट प्रणाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करती है, जहां बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार आर्थिक गतिविधि के लिए केंद्रीय हैं। जिन राष्ट्रों के पास पेटेंट की एक मजबूत प्रणाली है, उन्हें प्रौद्योगिकी और नवाचार के युग में नेताओं के रूप में देखा जाता है। यह प्रतिष्ठा ज्ञान वैश्वीकरण में उनकी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाती है।
पेटेंट अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उत्कर्ष को भी प्रोत्साहित करता है और आर्थिक विविधीकरण में योगदान देता है जो बदले में पारंपरिक उद्योगों पर निर्भरता को कम करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
पेटेंट संरक्षण की अवधि समाप्त होने के बाद क्या होता है?
न्यायमूर्ति राजगोपाल आयंगर समिति कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पेटेंट प्रणाली एक प्रकार की प्रतिपाद्य (क्विड प्रो कुओ) प्रणाली थी। इस प्रणाली में, आविष्कारक को पेटेंट अवधि समाप्त होने के बाद स्वतंत्र रूप से उपयोग किए जाने वाले आविष्कार के प्रकटीकरण के बदले बीस साल की निश्चित अवधि के लिए पेटेंट जारी करके एकाधिकार प्रदान किया जाता है। संरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी मूल पेटेंट धारक की अनुमति के बिना आविष्कार को बनाने, उपयोग करने, बेचने या आयात करने के लिए स्वतंत्र होगा।
आविष्कार के सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करने से अंततः बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा और नवाचार की अनुमति मिलेगी, क्योंकि अन्य कंपनियां और व्यक्ति आविष्कार पर निर्माण करने या नए और बेहतर उत्पाद या प्रक्रियाएं बनाने में सक्षम होंगे। दूसरा, एक बार पेटेंट समाप्त हो जाने और सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करने के बाद, पेटेंट धारक पेटेंट से संबंधित स्वतव भुगतान प्राप्त करना बंद कर सकता है। इसके अलावा, दूसरों के साथ कोई भी लाइसेंसिंग समझौता स्वचालित रूप से मिटा दिया जाएगा।
एक बार दिए गए पेटेंट की अवधि क्या है?
अधिनियम, 1970 की धारा 53 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत में प्रदान किए गए पेटेंट की अवधि 20 वर्ष है, जो पेटेंट आवेदन दायर करने की तारीख से शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि पेटेंट द्वारा दिए गए अनन्य अधिकार दाखिल करने की तारीख से 20 साल की अवधि के लिए वैध हैं, बशर्ते कि पेटेंट धारक सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें नवीकरण शुल्क का समय पर भुगतान और अन्य वैधानिक दायित्वों का अनुपालन शामिल है। इस 20 साल की अवधि के बाद, पेटेंट अधिकार समाप्त हो जाते हैं, और आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करता है, जिससे दूसरों को मूल पेटेंट धारक से अनुमति की आवश्यकता के बिना आविष्कार का उपयोग करने, बनाने या बेचने की अनुमति मिलती है।
पेटेंट के सदाबहार का क्या मतलब है?
आम आदमी के शब्दों में सदाबहार का मतलब कुछ ऐसा है जो जीवन भर चलेगा। पेटेंट कानून में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेटेंटकर्ता अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए अपने पेटेंट के जीवन का विस्तार कर सकता है। इस प्रयास में, पेटेंटकर्ता एक ही आविष्कार के विभिन्न भागों या पहलुओं को कवर करने के लिए कई पेटेंट दर्ज करता है। इसमें, आविष्कार की सुरक्षा अवधि को बीस साल की सीमा से आगे बढ़ाने के लिए कई अनुवर्ती (फॉलो अप) पेटेंट दायर किए जाते हैं। यह प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में आविष्कार के लिए की जा सकती है। हालांकि, यह दवा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है।
अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई खामी नहीं है जिसका उपयोग प्रतियोगी मूल पेटेंट को बायपास करने और पेटेंट सुरक्षा का उल्लंघन किए बिना प्रतिस्पर्धी उत्पाद या सेवा बनाने के लिए कर सकता है।
क्या पेटेंट रद्द किया जा सकता है?
अधिनियम, 1970 की धारा 64 पेटेंट के रद्द करने के आधारों से संबंधित है। निम्नलिखित कुछ आधारों का उल्लेख किया गया है:
- पेटेंट एक ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर प्रदान किया गया था जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदन करने का हकदार नहीं है।
- पेटेंट याचिकाकर्ता या किसी भी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन में गलत तरीके से प्राप्त किया गया था जिसके तहत या जिसके माध्यम से वह दावा करता है।
- पूर्ण विनिर्देश नया नहीं है, दावे की प्राथमिकता तिथि से पहले भारत में सार्वजनिक रूप से ज्ञात या सार्वजनिक रूप से उपयोग किया गया था।
- पूर्ण विनिर्देश के दावे स्पष्ट हैं या इसमें कोई आविष्कारशील कदम शामिल नहीं है।
- पूर्ण विनिर्देश का कोई भी दावा उपयोगी नहीं है।
- पेटेंट एक झूठे सुझाव या प्रतिनिधित्व पर प्राप्त किया गया था।
- पूर्ण विनिर्देश का कोई भी दावा इस अधिनियम के तहत पेटेंट योग्य नहीं है।
पेटेंट समापन का सिद्धांत क्या है?
पेटेंट समापन का सिद्धांत पेटेंटकर्ता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए सीमित करता है कि अन्य लोग एक आविष्कार को मूर्त रूप देने या युक्त लेख के साथ क्या कर सकते हैं। सिद्धांत के अनुसार, किसी पेटेंट वस्तु की पहली या प्रारंभिक अधिकृत बिक्री उस वस्तु के सभी पेटेंट अधिकारों को समाप्त कर देती है। हालांकि, यह केवल पेटेंटकर्ता के अधिकार को बेचे गए विशेष लेख तक सीमित करता है और खरीदार को पेटेंट किए गए आविष्कार की नई प्रतियां बनाने से रोकने के उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।
संदर्भ